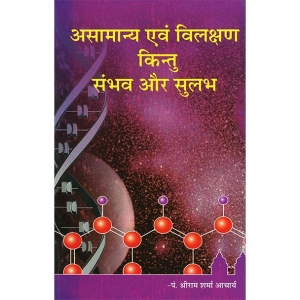असामान्य और विलक्षण किंतु संभव और सुलभ 
चाहे जो बन जाये इतनी भर ही छूट है
Read Scan Version
मानवी सत्ता, असुरता और देवत्व दोनों से मिलकर बनी है। परमात्मा ने यह छूट केवल मनुष्य को ही दी है कि वह चाहे तो दिव्य दैवी प्रवृत्तियां अपनाये अथवा आसुरी-पाशविक वृत्ति अपनाकर नरपशु से नरपिशाच बन जाये। यह चयन सुविधा मनुष्य के विवेक की परीक्षा के लिए ही मिली है। वह कौन सी प्रवृत्ति अपनाता है यह उसकी मनमर्जी की बात है। परन्तु जिस किसी भी वृत्ति को वह अपनाता है उसका पुरस्कार या दण्ड निश्चित रूप से मिलता है।
मनुष्य की प्रकृति में दोनों तत्त्व विद्यमान हैं। जिस पक्ष को समर्थन अवसर और पोषण मिलता है वही पक्ष सुदृढ़ होता जाता है। सद्गुण सद्भाव और सद् विचारों की दिव्य भावनाओं का अभ्यास मनुष्य को देवता बना देता है और इनकी पुष्टि होती जाती है तो व्यक्ति नर से नारायण बनता जाता है। इसके विपरीत यदि वह दुष्ट संगति, दुराचरण, आसुरी क्रियाकलाप और पाप प्रवृत्तियों को अपनाता है तो धीरे-धीरे निकृष्ट से निकृष्टतम बनता चला जाता है। पशु से भी बढ़कर पिशाच का रूप धारण करता है और जघन्य कृत्य करके ही उसके भीतर बैठा असुर मोद मनाता है। ऐसे कुकृत्य जिन्हें सुनकर ही एक सहृदय व्यक्ति कांप उठे वह उन नृशंस कृत्यों को अपने अहंकार की पूर्ति समझने लगता है।
1, 30 ई. में ट्रान्सलवानिया के पहाड़ी प्रदेशों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला काउण्ट ड्राक्युला ऐसा ही नर पिशाच था। उसने 1476 तक राज्य किया 46 वर्षों के इस शासन काल में उसने ऐसी-ऐसी अमानवीय क्रूरतायें बरतीं कि उसे इतिहासकारों ने ‘लाद दि इम्पेलर’ अर्थात् आदमी के शरीर को छेदने वाला कहा। जिस किसी भी व्यक्ति पर वह अप्रसन्न हो जाता उसे सजा देने के लिए वह क्रूरतम तरीका अपनाता था। वह लोगों को लकड़ी के बड़े-बड़े आदम कद खूंटों पर कीलों से ठोकवा देता और उनकी पीड़ा तथा तड़प को देखकर प्रसन्न होता था।
यह उसका मनोरंजन भी था। वह प्रायः अपने महल में प्रीतिभोज दिया करता। भोज की मेज के चारों ओर काठ की बनी सूलियों पर जीवित मनुष्यों के शरीर की कीलों से टंगे होते थे। लोग यातना और पीड़ा से चीखते-चिल्लाते रहते और उन्हें देखकर ड्राक्युला बड़ा आनन्द विभोर होता हुआ भोजन करता रहता। सड़ती लाशों और बासी खून की सड़ांध भरी बदबू में ड्राक्युला को जैसे महक-सी आती थी।
दरबार में भी वह इसी प्रकार सूलियों पर जीवित लोगों को कीलों से ठोकवा देता तथा शासन प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता रहता। दरबारी बड़े सहमे और डरे रहते थे क्योंकि इससे जरा भी विरोध या अरुचि दर्शाने का अर्थ था उनकी भी वही दशा। एक बार किसी नये दरबारी ने ड्राक्युला से कह दिया—इन लाशों से बहुत बदबू आती है। उसने ड्राक्युला को यह कार्य कहीं एकांत में करने की सलाह दी ताकि दरबार में आने वालों को दुर्गन्ध का सामना न करना पड़े। ड्राक्युला ने इस सुझाव को सुनकर जोरों से अट्टहास किया और बड़ा उल्लास व्यक्त करते हुए उसने तुरन्त आदेश दिया कि इस आदमी को भी एक खूंटे पर ठोक दिया जाय। वह दरबारी घबड़ा कर माफी मांगने लगा। जीवन दान की दया याचना करने लगा तो ड्राक्युला ने इस पर दयाभाव जताते हुए इतना भर किया कि उसका खूंटा कुछ ऊंचा गढ़वाया और उसे ऊंचे खूंटे पर जड़वा दिया। इस दया को जताते हुए उसने कहा था ‘अब तुम्हें कभी भी दूसरों की बदबू नहीं मिलेगी। घबड़ाने की जरूरत नहीं है।’
ड्राक्युला ने इस प्रकार क्रूरता पूर्वक नृशंस हत्यायें करने के नये-नये ढंग ईजाद किये थे। इसमें उसे बड़ा आनन्द आता था। हत्याओं के एक ही तरीके से जब वह ऊब जाता तो दूसरे तरीके भी अपनाने लगता। कई बार वह दूध पीते हुए बच्चों को उनकी माताओं के सीने पर ही कील से जड़वा देता। मां-बाप के सामने ही उनके अबोध और प्यारे बच्चों को मारकर उन्हें अपने बच्चों का मांस खाने के लिए मजबूर कर देता। एक बार उसने अपने राज्य के सभी गरीब, बूढ़े और बीमार लोगों को सेना द्वारा इकट्ठा कराया तथा उन्हें जिन्दा जलवा दिया।
ड्राक्युला के नाम और आतंक का इतना दबदबा था कि उसकी चर्चा आज भी ट्रांसलवानियां में होती है तो लोग मारे दहशत के चर्चा वहीं बन्द करने का आग्रह करने लगते हैं। इतिहासकारों ने ड्राक्युला को अब तक के विश्व का सर्वाधिक क्रूर, नृशंस और अत्याचारी शासक माना है।
1620 से 1666 तक लिपजिंग (जर्मनी) के सेशन कोर्ट में न्यायाधीश रहा बेनेडिक्ट कार्पजे बड़ी कठोर और क्रूर प्रकृति का था। लोग उसे भी ड्राक्युला का अवतार बताते हैं। जो भी हो परन्तु उसका जीवन ड्राक्युला से अद्भुत समानता रखता था। ड्राक्युला ने 46 वर्ष तक शासन किया, कार्पजे भी 46 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। उसने इस काल में 30 हजार पुरुषों और 22 हजार स्त्रियों को फांसी पर चढ़ाया छोटे से छोटे अपराध, जुआ, चोरी और उठाईगीरी तक में वह मृत्यु दण्ड देता था। जैसे मृत्युदण्ड से नीची सजा कोई हो ही नहीं। स्त्रियों को तो उसने जादू-टोने के संदेह तक में पकड़वा कर फांसी पर चढ़ा दिया।
कार्पजे ने औसतन प्रतिदिन पांच व्यक्तियों को फांसी पर चढ़वाया और फांसी देखने के लिए वह स्वयं वध-स्थल पर पहुंचता। फांसी लगने का दृश्य देखने में उसे बहुत रस आता था। उसके साथ ही वह यह व्यवस्था भी देखता कि मृतकों का मांस खाने के लिए शिकारी कुत्ते तथा दूसरे जानवर, यथा समय पहुंचे हैं अथवा नहीं। दया या क्षमा शब्द तो जैसे कार्पजे ने कहीं सीखा ही नहीं था फिर भी वह अपने आपको धार्मिक कहता था।
निष्ठुर नृशंसता के ये दो इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हैं जिनमें केवल आदमी को मरते हुए देखने का आनन्द लिया जाता रहा। व्यक्तिगत जीवन में भी यह नृशंसता समय-समय पर घुलती रहती है और सामाजिक जीवन में भी विष घोलती रहती है। लेकिन एक बात तय है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की अमानवीय, क्रूरता को छोटे या बड़े किसी भी रूप में अपनाते हैं वे जीवन में कभी भी चैन से नहीं बैठ पाते हैं।
इस शताब्दी में नृशंस सामूहिक हत्याओं के लिए हिटलर का नाम बड़ी घृणा और तिरस्कार के साथ लिया जाता है। उसने लाखों निरपराध व्यक्तियों को मरवाया। परन्तु वह जीवन भर चैन से नहीं बैठ सका, यहां तक कि अपनी छाया से, अपने पदचाप की प्रतिध्वनि तक से डरता रहा। कहते हैं कि वह इतना सशंकित रहता था कि रात में चार-पांच घण्टे की नींद लेते समय भी तीन-चार बार उठ बैठता और अपने सिरहाने रखी रिवाल्वर तथा अन्य सुरक्षा प्रबन्धों की जांच करके देखता।
ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी उसी प्रकृति के बने रहते हैं। अशान्त, व्यथित और आत्म प्रताड़ना से आन्दोलित उनका जीवन नाटकीय बन जाता है। बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के वे मरने के बाद भी प्रेत, पिशाच बनकर लोगों को अपने दुष्ट आचरण द्वारा सताते रहते हैं।
इटली के तानाशाह मुसोलिनी के सम्बन्ध में विख्यात है कि वह मरने के बाद प्रेत बनकर अपने खजाने की रखवाली करता रहा है। युद्ध में हारने के बाद वह अपनी जान बचाकर स्विट्जरलैंड की तरफ भागा था। अरबों रुपयों की सम्पत्ति, सोने की छड़, हीरे, जवाहरात, पौण्ड, पेंस और डॉलरों के रूप में उसके पास जमा थी। लेकिन वह भागने में सफल नहीं हुआ और कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा गोली से उड़ा दिया।
इसके बाद उसने प्रेत, पिशाच का रूप धारण कर लिया और अपने खजाने की रखवाली करने लगा। अशरीरी होने के कारण खुद तो वह खजाने का लाख उठा नहीं सकता था, लेकिन वह दूसरों को भी उसका लाभ नहीं उठाने देना चाहता था। कहा जाता है कि उसी ने प्रेत, पिशाच बनकर खुद अपना खजाना छुपाया और उसकी रखवाली करने लगा। जिनने भी उसका पता लगाने की कोशिश की मुसोलिनी के प्रेत ने उनके प्राण लेकर ही छोड़े। उस खजाने की ढुंढ़वाने और प्राप्त करने के लिए सरकार ने कितनी ही समतियां गठित कीं परन्तु सभी खोजी दल अकाल कवलित हो गये।
मरने के बाद उस प्रेत, पिशाच पर क्या बीतती होगी यह तो कहा नहीं जा सकता परन्तु व्यक्ति के अपने नृशंस क्रूर कर्म उसे स्वयं तड़पा-तड़पा कर मारते हैं। ट्रांसलवानिया के शासक काउण्ट ड्राक्युला ने अपने जीवनकाल में जिस प्रकार लोगों की नृशंस हत्यायें की उससे भी भयंकर तरीके से उसे मारा गया। तुर्की सेनाओं ने जब ट्रांसलवानिया को जीतकर ड्राक्युला को बन्दी बना लिया तो उसके शरीर से रोज मांस का एक टुकड़ा काट लिया जाता और वही उसे कच्चा चबाने के लिये मजबूर किया जाता।
जर्मनी के नृशंस-क्रूर न्यायाधीश कार्पजे को कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ लिया जिनके सम्बन्धियों को निरपराध होते हुए भी उसने सजा दी थी और फांसी पर चढ़वाया था। उन लोगों ने कार्पजे को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जहां हजारों बिच्छू पहले से ही रख दिये गये थे। कोई तीन दिन में उसकी मृत्यु हुई। उस कोठरी में से कार्पजे की आवाज आना बन्द हुई तब लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसके शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां बिच्छुओं ने दंश नहीं लिया हो।
यह तो हुई बाहरी दण्ड व्यवस्था प्रतिशोध परक वृत्तान्त। इनसे बचा भी जा सकता है। परन्तु परमात्मा ने एक ऐसा न्यायाधीश इसी शरीर में बिठा दिया है जो व्यक्ति के कर्मों को देखता रहता है और यथा समय दण्डित भी करता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय अपने जीवन भर के कर्मों की याद आती है और वे स्मृतियां व्यक्ति को दग्ध करने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पराभव के समय व्यक्ति को अपने सारे क्रूर कर्म याद आते हैं और वह अपने ही कर्मों के प्रेत से डरकर अपने आपको उत्पीड़न करने लगता है।
सन् 1918-19 की घटना है। रूस में कम्युनिस्ट क्रान्ति हो चुकी थी। जारशाही के स्तम्भ एक-एक कर ढहते जा रहे थे और लोग जो निरीह गरीब तबके का निर्ममता के साथ शोषण करते रहे थे, एक-एक कर भाग रहे थे अपने बचाव के लिए। ऐसे ही भागने वाले व्यक्तियों में एक था करेलिया प्रदेश का जागीरदार इवान। वह अपनी पत्नी अन्ना, बेटी काल्या और पुत्र कोल्या के साथ करेलिया के बीहड़ प्रदेश में नदी के तट पर भागते हुए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे।
सेण्ट पीटर्स वर्ग से कुछ मील दूर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी एक काटेज में उन्होंने शरण ली। उन लोगों के साथ उनका एक पुराना सेवक बूढ़ा मल्लाह भी था। इवान ने अपनी वासना-पूर्ति के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ अनाचार किया था, उनमें से कइयों ने तो आत्महत्या कर ली थी, अनेक अबोध बालिकायें इस क्रूर कर्म को सहन न कर पाने के कारण मर गयीं। यही हाल अन्ना का था, अपने चरित्र पर परदा पड़ा रहे इसलिए उसने अपने बाप और भाई तक को मरवा डाला था।
इसके अलावा भी जागीरदार ने हजारों निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था। उस काटेज में दोनों को अपने अतीत की याद आने लगी। संयोग की बात यह है कि जिस काटेज में उन्होंने शरण ली, वह काटेज कभी इवान का विलास महल रह चुका था। वहां का एक-एक पत्थर इवान के क्रूर कर्मों का साक्षी था। ये क्रूर कर्म इतने वीभत्स और भयावह रूप में याद आ रहे थे कि वे सब लोग जिन्हें उसने सताया था, प्रेत बनकर उससे बदला लेने के लिए उतारू लगने लगे। इस स्थिति में इवान ने अपनी पत्नी, बच्चों को बूढ़े मल्लाह के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में अन्ना इतनी विक्षिप्त हो उठी कि अपने कपड़े फाड़ने लगी, बाल नोंचने लगी और नदी पार करते समय नाव में से कूद पड़ी।
इवान का भी यही हाल हुआ। उसने भी आत्म प्रताड़ना या अतीत में किये गये क्रूर कर्मों की स्मृति से बुरी तरह भयभीत होकर नेवा झील में कूदकर आत्म-हत्या करली। स्मरणीय है दोनों पति-पत्नी अपनी क्रूरता के शिकार व्यक्तियों को नदी, झील में ही फेंका करते थे। शासन और सेना से भले ही वह बच गये परन्तु अपनी अन्तरात्मा में बैठे न्यायाधीश से बचना कहां सम्भव रहा? तत्त्वविदों का कथन है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है। वह चाहे तो देवता भी बन सकता है और यदि चाहे तो नरपिशाच भी। परन्तु इनके परिणामों में चुनाव जैसी कोई स्वतन्त्र नहीं है। जिन्होंने भी असुरता पकड़ी और नृशंसता अपनायी उन्हें अन्ततः उसका दण्ड भुगतना ही पड़ा। भले ही वे तत्काल अपने अहंकार को सन्तुष्ट कर सके हों पर परिणाम में उससे भी भयंकर यातना तथा अन्त में उनकी यंत्रणा दायक स्मृतियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला पाया है।
आत्मचेतना का उपयोग
प्राचीन काल में प्रकृति परमात्मा की इसी नियम व्यवस्था का लाभ उठाकर ऋषि-महर्षियों ने आत्मसत्ता की सामर्थ्य का लाभ उठाया था। आज भी उसके प्रमाण कभी कदा देखने को मिल जाते हैं। एक समय था जब आधुनिक विज्ञान और आत्मविद्या कभी भी न मिल सकने वाले दो परस्पर विरोधी बिन्दु माने जाते थे। इसी कारण विज्ञान की प्रगति के साथ आध्यात्मिक अवमानना हुई। किन्तु आधुनिक विज्ञान भी बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी स्थिति में आ गया है जब उसे यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि क्या शरीर ही आत्मा है या आत्मा की अभिव्यक्ति के लिये शरीर अपर्याप्त माध्यम नहीं? मनुष्य की मस्तिष्कीय चेतना की भौतिक परिधि और उसकी विराट् अवस्था दोनों के व्यापक अध्ययन से धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि सारे शरीर में मस्तिष्क के विद्यमान होने की तरह विराट् चेतना सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। शरीर उसका एक स्टेशन और मन्दिर मात्र है जिसमें वह अपने अंश या जीव रूप में कुछ क्षण विश्राम के लिये आता है। उसका अन्तिम लक्ष्य विभु या विराट् बनना है। इस उद्देश्य की पूर्ति न होने तक सन्तोष नहीं होता।
मनुष्य की चिंतन शक्ति, भावनाओं, संवेदनाओं को मात्र रासायनिक संवेग मानकर मनुष्य जीवन को नितान्त भौतिक मानने की भूल थोड़े से वैज्ञानिकों ने की है। अधिकांश ने या तो अत्यन्त गूढ़ कहकर निष्कर्ष निकालने का विचार ही त्याग दिया या फिर श्रद्धापूर्वक उनने यही स्वीकार किया कि मानवीय चेतना का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। वह भौतिकीय तत्त्वों का सम्मिलन मात्र नहीं, अपितु विराट् चेतना का ही अंश है। वह शरीर रूप नाम का पिंड मात्र नहीं, अनादि अनन्त गुण वाला चेतन तत्त्व है। शरीरों का इन्द्रियों का विकास उसकी इच्छानुसार, उसके संकल्प के आधार पर हुआ है।
भौतिक विज्ञान के जो पण्डित स्नायु-तन्त्र (नाड़ी मण्डल) को ही आत्मा मानते और उन्हीं से विचारों को उद्भूत हुआ मानते हैं उनमें जर्मनी के शरीर विज्ञानी डा. काल ह्वाक्ट तथा डा. टेन्डाल आदि प्रमुख हैं। अपने सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने अनेक प्रयोग शरीर पर किये। स्नायु-मण्डल की विस्तृत खोज की। उन्होंने उस गति की माप की जो शरीर में किसी अंग पर आघात के बाद उस अंग से भाव सन्देश के रूप में मन तक और मन से शरीर के किसी अंग तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क-बोध की सूक्ष्मता का भी पता लगाया तथा विद्युत आवेश देकर उन संदेशों को घटाने-बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की विचारों की उत्पत्ति को उन्होंने कहा यह मस्तिष्क की वैसी ही उपज होते हैं जैसे यकृत की पित्त। हालांकि अब तक वैज्ञानिक मस्तिष्क के गहन अन्धकार में झांककर जितना जान सके हैं वह अधिकतम 13 प्रतिशत है। मस्तिष्क के शेष 87 प्रतिशत भाग की कोई जानकारी नहीं है। इतनी कम जानकारी को पूर्णता की संज्ञा देना वैसे ही अविवेकपूर्ण कहा जायेगा।
फिर कुछ ऐसी घटनायें और प्रसंग भी आये दिन आते रहते हैं जो इस वैज्ञानिक मान्यता के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिक उन कारणों की कोई व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ इटली में गियोवानी गलान्ती नामक एक ऐसा बालक था जो रात के अंधेरे में भी पढ़ सकता था। 1928 में उसे इसी स्वास्थ्य परीक्षा के बाद अमेरिका नहीं जाने दिया गया था। पढ़ते समय मुख्य कार्य मस्तिष्क करता है और कोई भी मस्तिष्क प्रकाश के बिना पढ़ नहीं सकता, फिर इस बालक में यह क्षमता कहां से आई?
स्लाटलैण्ड में जेम्स क्रिस्टन नाम के एक बालक ने 12 वर्ष में ही अरबी, ग्रीक, यहूदी तथा फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषायें सीख ली थीं। 20 वर्ष तक वह विज्ञान की सभी भाषाओं का पण्डित हो गया था। उसके और सामान्य व्यक्ति के आहार और जीवन क्रम में जब कोई विशेष अन्तर नहीं था, तब बौद्धिक क्षमता में आकाश-पाताल जैसे अन्तर का कारण क्या हो सकता है? फ्रांस में जन्मे लुईस कार्डक 4 वर्ष की आयु के थे तभी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी तथा अन्य योरोपीय भाषायें बोल लेते थे। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि वह 6 माह की आयु में ही बाइबिल पढ़ लेते थे। 6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर कोई भी प्रोफेसर गणित, इतिहास और भूगोल में इनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमतायें इतने अधिक अध्ययन और अभ्यास से विकसित हो पाती हैं और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार जिन्हें पदार्थ की परिणति होना चाहिये थीं, वह शारीरिक विकास के अभाव में ही इतने विकास तक कैसे जा पहुंचीं?
ब्लेइस पास्कल ने 12 वर्ष की आयु में ही ध्वनि-शास्त्र पर निबन्ध प्रस्तुत कर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया था। जीन फिलिप बेरोटियर को 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर आफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि दिन याद कराने की देर होती थी उस दिन की व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें भी टेप की भांति दुहरा सकते थे। जोनी नामक आस्ट्रेलियाई बालक को जब तीन वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो वह उसी दिन से 8वीं कक्षा के छात्रों की पुस्तकें पढ़ लेता था। उसे हाई स्कूल में केवल इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सका क्यों उस समय उसकी आयु कुल 5 वर्ष थी जबकि निर्धारित आयु 12 वर्ष न्यूनतम थी।
कोई भी अल्पबुद्धि व्यक्ति यह स्पष्ट समझ सकता है कि यह असामान्य ज्ञान पूर्व जन्मों के ही संस्कार हो सकते हैं। हमारे मनीषी निरन्तर स्वाध्याय की आवश्यकता अनुमोदित करते रहे और यह बताते रहे कि ज्ञान आत्मा की भूख-प्यास की तरह है। उससे उसका विकास होता है। यह बात समझ में आने वाली है कि चेतना का विकास ज्ञान साधना से ही सम्भव है जो अद्भुत क्षमता के रूप में हर किसी को मिलती है। बालकों के आहार, वातावरण, पोषण आदि की समान सुविधायें होने पर भी बौद्धिक असमानता इन्हीं भारतीय मान्यताओं की समर्थक हैं।
इटली के डा. लोम्ब्रोसो जिन्होंने एक समय एक प्रतिष्ठापना दी थी कि रचना विज्ञान की दृष्टि से एक पागल और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों में समरूपता होती है। इस बात को भौतिकवादियों ने बहुत अधिक उछाला, किन्तु वे यह भूल गये कि देखने में नमक और शक्कर दोनों में समानता दिखाई देने पर भी उनके गुणों में इतना अन्तर होता है कि एक के भाव 5 रु. किलो होते हैं तो दूसरे के 10 पैसे किलो। प्रतिभाशाली व्यक्तियों, आध्यात्मिक, धार्मिक संतों के विचारों में रचनात्मक जागरूकता और मार्गदर्शन की क्षमता होती है। उन्होंने सैकड़ों लोगों के जीवन में शांति, सुरुचि और सुव्यवस्था दी जबकि पागल के विचार अस्त व्यस्त होते हैं। उसे लोग दुत्कारते ही हैं, उसकी सुनता कोई नहीं।
लोम्ब्रोसी के उक्त प्रतिपादन का खण्डन अनेक वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। डा. मोर्शले ने उपरोक्त मत से असहमति व्यक्त की है और लिखा है कि सामान्य मस्तिष्क में दुनियादारी की प्रवृत्ति तो होती है, किन्तु सूक्ष्म चिन्तनशक्ति असाधारण लोगों में ही होती है।
मैडम ब्लैवटस्की का कथन है कि मस्तिष्क उस वीणा व वायलिन की तरह है जिसके तार को जितना अधिक खींचा व कसा जायेगा ध्वनि कम्पन उतने ही सूक्ष्म और मोहक होंगे। असामान्य मस्तिष्क की असामान्य उपलब्धियां ऐसी ही हैं तार कसने में उसके टूटने का भय होता है। इसलिए उसे धीरे-धीरे सावधानी से कसते हैं। मस्तिष्क को जिन साधनों (योग विद्या) से सूक्ष्म तत्वग्राही और संवेदनशील बनाया जाता है उनकी भी यही प्रवृत्ति होती है। एकाएक कठोर अभ्यास—पागल और विक्षिप्त कर भी सकते हैं, इसलिए साधना का क्रम मार्ग-दर्शकों की देख-रेख में धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। शारीरिक अभ्यास, उपवास आदि से शरीर शोधन, विचारों में प्रकाश अवधारणा आदि से ही उच्च क्षमताएं विकसित होती हैं। योगियों पर कोई स्नायविक दबाव नहीं पड़ता, कोई बीमारी नहीं होती। अतएव सूक्ष्म विचारों की महत्त्व के साथ-साथ योग-साधनाओं की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। चिंतन के सूक्ष्मतर होने से ज्ञान चेतना के कोश परस्पर जुड़ते हुए चले जाते हैं और सामान्य मस्तिष्क जो सन्देश, प्रेरणायें, अनुभूतियां नहीं गृहण कर पाते उनके लिए सुलभ हो जाती हैं। सर आलिवर लाज ने भी अपनी बौद्धिक क्षमतायें इसी आधार पर विकसित की थीं और यह माना था कि हमारी ज्ञान चेतना पदार्थ जन्य न होकर विराट् चेतना का ही एक अंश और अंग है। जब तक इस बात को नहीं समझते तब तक हमारे दृष्टिकोण भी भौतिकतावादी बने रहते हैं। तब पाप-पुण्य में कोई अन्तर ही नहीं रहता, नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं होता। आज जो सर्वत्र पीड़ा और पतन के दृश्य हैं, स्वार्थ संकीर्णता ने पुण्य-परमार्थ को दबोच रखा है, वह उसी मान्यता का दुष्परिणाम है।
पूर्वी मनोविज्ञान या भारतीय दर्शन के पीछे शोधों की एक लम्बी विज्ञान सम्मत श्रृंखला है जबकि पश्चिमी मनोविज्ञान अभी 30-40 वर्ष का बालक मात्र है जो सतह पर खड़ा स्नान करता है। उसमें इतनी क्षमता भी नहीं कि गहरे जाकर गोता लगा सके। इसीलिए वह जितने समाधान प्रस्तुत करता है उतने ही प्रश्न और समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। ऊपर मस्तिष्क की जिन अदम्य क्षमताओं का वर्णन किया गया है उन्हें कुछ देर के लिये भूल भी जायें तो भी जब मस्तिष्क सामान्य नहीं होता तब भी चेतन क्रियायें चलती रहती हैं। न केवल जागृत अवस्था में अपितु स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था में भी चेतना बनी रहती है उसका भी समाधान आवश्यक है। डा. ड्यूप्रेल ने अपनी पुस्तकों में ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिनसे यह सिद्ध होता है कि समय या अनुभूति के एक सेकेंड के करोड़वें भाग में ही महाकाल या अनेक वर्षों में हुए ज्ञान की अनुभूति कैसे सम्भव हो जाती है। इसका अर्थ तो स्पष्टतः यही होता है कि कोई एक ऐसी चेतना है जो विराट् है और उसके लघुत्तम अंश में भी वही सम्भावनायें सन्निहित हैं। अपनी पुस्तक में डा. प्रेल ने एक व्यक्ति के स्वप्न का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस व्यक्ति की गर्दन का एक उंगली से स्पर्श किया गया। उसकी नींद टूट गई। जब उससे अनुभव के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने स्वप्न देखा कि मैंने किसी की हत्या करदी, उस व्यक्ति के घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने पकड़ा, जेल भेजा, मुकदमा चला, वकील की जिरह हुई, मुझे फांसी की सजा हो गई। नियम समय पर जल्लाद आया, उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और नींद टूट गई।
डा. प्रेल लिखते हैं जिस तरह ज्ञान के अंश में ही विराट्-काल व्याप्त होने का यह उदाहरण है उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात है सम्मोहन की अवस्था में (हिप्नोटिज्म) व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसे अपनी स्थिति का भी बोध नहीं रहता, आंखें देख नहीं सकतीं, कान सुन नहीं सकते, पलकें तीव्र विद्युत प्रकाश में भी सिकुड़ती हैं, त्वचा स्पर्श ज्ञान से शून्य हो जाती है। हृदय की धड़कन बन्द-सी हो जाती है, अत्यन्त संवेदनशील यंत्रों से ही जीवन का बोध होता है। कार्बन तत्त्व अत्यधिक बढ़ जाने से मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो जाना चाहिए था। जड़ता, अगति या मृत्यु हो जानी चाहिए थी किन्तु तब ज्ञान की क्षमतायें जागृति से भी अनेक गुनी अधिक बढ़ जाती हैं। अर्थात् सम्मोहन की अवस्था में बाल्यावस्था की जो घटनायें याद नहीं रहतीं वे भी स्मरण शक्ति में आ जाती है। सामान्य स्थिति में कोई पुस्तक का एक पैराग्राफ पढ़े तो तीव्र बुद्धि व्यक्ति ही उसके कुछ शब्द दोहरा सकते हैं पर सम्मोहित अवस्था में तो यदि भाषा उसकी पढ़ी हुई नहीं तो भी अक्षर-ब-अक्षर दोहरा सकता है। जागृत अवस्था में आंख की शक्ति सीमित होती है, किन्तु उस स्थिति में कमरे में बन्द रहकर भी सैकड़ों मील दूर की वस्तुएं तक दिखाई देती हैं यह सब कैसे सम्भव है? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्म-चेतना विराट् चेतना का ही अंश है जिसमें असीम ज्ञान की शक्ति, अद्वितीय क्षमताओं की सम्भावना सन्निहित है। भूत, भविष्य और वर्तमान उसी में अवस्थित हैं, वह पदार्थ से परे है तथा उसे जानने में ही जीवन की सार्थकता है। योग-साधना, ध्यान-धारणा और-साधन अभ्यासों द्वारा इन्हीं शक्ति-केन्द्रों को जागृत किया जाता है तथा दिव्य-शक्ति सम्पन्न हुआ जाता है।
मनुष्य की प्रकृति में दोनों तत्त्व विद्यमान हैं। जिस पक्ष को समर्थन अवसर और पोषण मिलता है वही पक्ष सुदृढ़ होता जाता है। सद्गुण सद्भाव और सद् विचारों की दिव्य भावनाओं का अभ्यास मनुष्य को देवता बना देता है और इनकी पुष्टि होती जाती है तो व्यक्ति नर से नारायण बनता जाता है। इसके विपरीत यदि वह दुष्ट संगति, दुराचरण, आसुरी क्रियाकलाप और पाप प्रवृत्तियों को अपनाता है तो धीरे-धीरे निकृष्ट से निकृष्टतम बनता चला जाता है। पशु से भी बढ़कर पिशाच का रूप धारण करता है और जघन्य कृत्य करके ही उसके भीतर बैठा असुर मोद मनाता है। ऐसे कुकृत्य जिन्हें सुनकर ही एक सहृदय व्यक्ति कांप उठे वह उन नृशंस कृत्यों को अपने अहंकार की पूर्ति समझने लगता है।
1, 30 ई. में ट्रान्सलवानिया के पहाड़ी प्रदेशों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला काउण्ट ड्राक्युला ऐसा ही नर पिशाच था। उसने 1476 तक राज्य किया 46 वर्षों के इस शासन काल में उसने ऐसी-ऐसी अमानवीय क्रूरतायें बरतीं कि उसे इतिहासकारों ने ‘लाद दि इम्पेलर’ अर्थात् आदमी के शरीर को छेदने वाला कहा। जिस किसी भी व्यक्ति पर वह अप्रसन्न हो जाता उसे सजा देने के लिए वह क्रूरतम तरीका अपनाता था। वह लोगों को लकड़ी के बड़े-बड़े आदम कद खूंटों पर कीलों से ठोकवा देता और उनकी पीड़ा तथा तड़प को देखकर प्रसन्न होता था।
यह उसका मनोरंजन भी था। वह प्रायः अपने महल में प्रीतिभोज दिया करता। भोज की मेज के चारों ओर काठ की बनी सूलियों पर जीवित मनुष्यों के शरीर की कीलों से टंगे होते थे। लोग यातना और पीड़ा से चीखते-चिल्लाते रहते और उन्हें देखकर ड्राक्युला बड़ा आनन्द विभोर होता हुआ भोजन करता रहता। सड़ती लाशों और बासी खून की सड़ांध भरी बदबू में ड्राक्युला को जैसे महक-सी आती थी।
दरबार में भी वह इसी प्रकार सूलियों पर जीवित लोगों को कीलों से ठोकवा देता तथा शासन प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता रहता। दरबारी बड़े सहमे और डरे रहते थे क्योंकि इससे जरा भी विरोध या अरुचि दर्शाने का अर्थ था उनकी भी वही दशा। एक बार किसी नये दरबारी ने ड्राक्युला से कह दिया—इन लाशों से बहुत बदबू आती है। उसने ड्राक्युला को यह कार्य कहीं एकांत में करने की सलाह दी ताकि दरबार में आने वालों को दुर्गन्ध का सामना न करना पड़े। ड्राक्युला ने इस सुझाव को सुनकर जोरों से अट्टहास किया और बड़ा उल्लास व्यक्त करते हुए उसने तुरन्त आदेश दिया कि इस आदमी को भी एक खूंटे पर ठोक दिया जाय। वह दरबारी घबड़ा कर माफी मांगने लगा। जीवन दान की दया याचना करने लगा तो ड्राक्युला ने इस पर दयाभाव जताते हुए इतना भर किया कि उसका खूंटा कुछ ऊंचा गढ़वाया और उसे ऊंचे खूंटे पर जड़वा दिया। इस दया को जताते हुए उसने कहा था ‘अब तुम्हें कभी भी दूसरों की बदबू नहीं मिलेगी। घबड़ाने की जरूरत नहीं है।’
ड्राक्युला ने इस प्रकार क्रूरता पूर्वक नृशंस हत्यायें करने के नये-नये ढंग ईजाद किये थे। इसमें उसे बड़ा आनन्द आता था। हत्याओं के एक ही तरीके से जब वह ऊब जाता तो दूसरे तरीके भी अपनाने लगता। कई बार वह दूध पीते हुए बच्चों को उनकी माताओं के सीने पर ही कील से जड़वा देता। मां-बाप के सामने ही उनके अबोध और प्यारे बच्चों को मारकर उन्हें अपने बच्चों का मांस खाने के लिए मजबूर कर देता। एक बार उसने अपने राज्य के सभी गरीब, बूढ़े और बीमार लोगों को सेना द्वारा इकट्ठा कराया तथा उन्हें जिन्दा जलवा दिया।
ड्राक्युला के नाम और आतंक का इतना दबदबा था कि उसकी चर्चा आज भी ट्रांसलवानियां में होती है तो लोग मारे दहशत के चर्चा वहीं बन्द करने का आग्रह करने लगते हैं। इतिहासकारों ने ड्राक्युला को अब तक के विश्व का सर्वाधिक क्रूर, नृशंस और अत्याचारी शासक माना है।
1620 से 1666 तक लिपजिंग (जर्मनी) के सेशन कोर्ट में न्यायाधीश रहा बेनेडिक्ट कार्पजे बड़ी कठोर और क्रूर प्रकृति का था। लोग उसे भी ड्राक्युला का अवतार बताते हैं। जो भी हो परन्तु उसका जीवन ड्राक्युला से अद्भुत समानता रखता था। ड्राक्युला ने 46 वर्ष तक शासन किया, कार्पजे भी 46 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। उसने इस काल में 30 हजार पुरुषों और 22 हजार स्त्रियों को फांसी पर चढ़ाया छोटे से छोटे अपराध, जुआ, चोरी और उठाईगीरी तक में वह मृत्यु दण्ड देता था। जैसे मृत्युदण्ड से नीची सजा कोई हो ही नहीं। स्त्रियों को तो उसने जादू-टोने के संदेह तक में पकड़वा कर फांसी पर चढ़ा दिया।
कार्पजे ने औसतन प्रतिदिन पांच व्यक्तियों को फांसी पर चढ़वाया और फांसी देखने के लिए वह स्वयं वध-स्थल पर पहुंचता। फांसी लगने का दृश्य देखने में उसे बहुत रस आता था। उसके साथ ही वह यह व्यवस्था भी देखता कि मृतकों का मांस खाने के लिए शिकारी कुत्ते तथा दूसरे जानवर, यथा समय पहुंचे हैं अथवा नहीं। दया या क्षमा शब्द तो जैसे कार्पजे ने कहीं सीखा ही नहीं था फिर भी वह अपने आपको धार्मिक कहता था।
निष्ठुर नृशंसता के ये दो इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हैं जिनमें केवल आदमी को मरते हुए देखने का आनन्द लिया जाता रहा। व्यक्तिगत जीवन में भी यह नृशंसता समय-समय पर घुलती रहती है और सामाजिक जीवन में भी विष घोलती रहती है। लेकिन एक बात तय है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की अमानवीय, क्रूरता को छोटे या बड़े किसी भी रूप में अपनाते हैं वे जीवन में कभी भी चैन से नहीं बैठ पाते हैं।
इस शताब्दी में नृशंस सामूहिक हत्याओं के लिए हिटलर का नाम बड़ी घृणा और तिरस्कार के साथ लिया जाता है। उसने लाखों निरपराध व्यक्तियों को मरवाया। परन्तु वह जीवन भर चैन से नहीं बैठ सका, यहां तक कि अपनी छाया से, अपने पदचाप की प्रतिध्वनि तक से डरता रहा। कहते हैं कि वह इतना सशंकित रहता था कि रात में चार-पांच घण्टे की नींद लेते समय भी तीन-चार बार उठ बैठता और अपने सिरहाने रखी रिवाल्वर तथा अन्य सुरक्षा प्रबन्धों की जांच करके देखता।
ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी उसी प्रकृति के बने रहते हैं। अशान्त, व्यथित और आत्म प्रताड़ना से आन्दोलित उनका जीवन नाटकीय बन जाता है। बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के वे मरने के बाद भी प्रेत, पिशाच बनकर लोगों को अपने दुष्ट आचरण द्वारा सताते रहते हैं।
इटली के तानाशाह मुसोलिनी के सम्बन्ध में विख्यात है कि वह मरने के बाद प्रेत बनकर अपने खजाने की रखवाली करता रहा है। युद्ध में हारने के बाद वह अपनी जान बचाकर स्विट्जरलैंड की तरफ भागा था। अरबों रुपयों की सम्पत्ति, सोने की छड़, हीरे, जवाहरात, पौण्ड, पेंस और डॉलरों के रूप में उसके पास जमा थी। लेकिन वह भागने में सफल नहीं हुआ और कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा गोली से उड़ा दिया।
इसके बाद उसने प्रेत, पिशाच का रूप धारण कर लिया और अपने खजाने की रखवाली करने लगा। अशरीरी होने के कारण खुद तो वह खजाने का लाख उठा नहीं सकता था, लेकिन वह दूसरों को भी उसका लाभ नहीं उठाने देना चाहता था। कहा जाता है कि उसी ने प्रेत, पिशाच बनकर खुद अपना खजाना छुपाया और उसकी रखवाली करने लगा। जिनने भी उसका पता लगाने की कोशिश की मुसोलिनी के प्रेत ने उनके प्राण लेकर ही छोड़े। उस खजाने की ढुंढ़वाने और प्राप्त करने के लिए सरकार ने कितनी ही समतियां गठित कीं परन्तु सभी खोजी दल अकाल कवलित हो गये।
मरने के बाद उस प्रेत, पिशाच पर क्या बीतती होगी यह तो कहा नहीं जा सकता परन्तु व्यक्ति के अपने नृशंस क्रूर कर्म उसे स्वयं तड़पा-तड़पा कर मारते हैं। ट्रांसलवानिया के शासक काउण्ट ड्राक्युला ने अपने जीवनकाल में जिस प्रकार लोगों की नृशंस हत्यायें की उससे भी भयंकर तरीके से उसे मारा गया। तुर्की सेनाओं ने जब ट्रांसलवानिया को जीतकर ड्राक्युला को बन्दी बना लिया तो उसके शरीर से रोज मांस का एक टुकड़ा काट लिया जाता और वही उसे कच्चा चबाने के लिये मजबूर किया जाता।
जर्मनी के नृशंस-क्रूर न्यायाधीश कार्पजे को कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ लिया जिनके सम्बन्धियों को निरपराध होते हुए भी उसने सजा दी थी और फांसी पर चढ़वाया था। उन लोगों ने कार्पजे को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जहां हजारों बिच्छू पहले से ही रख दिये गये थे। कोई तीन दिन में उसकी मृत्यु हुई। उस कोठरी में से कार्पजे की आवाज आना बन्द हुई तब लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसके शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां बिच्छुओं ने दंश नहीं लिया हो।
यह तो हुई बाहरी दण्ड व्यवस्था प्रतिशोध परक वृत्तान्त। इनसे बचा भी जा सकता है। परन्तु परमात्मा ने एक ऐसा न्यायाधीश इसी शरीर में बिठा दिया है जो व्यक्ति के कर्मों को देखता रहता है और यथा समय दण्डित भी करता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय अपने जीवन भर के कर्मों की याद आती है और वे स्मृतियां व्यक्ति को दग्ध करने लगती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पराभव के समय व्यक्ति को अपने सारे क्रूर कर्म याद आते हैं और वह अपने ही कर्मों के प्रेत से डरकर अपने आपको उत्पीड़न करने लगता है।
सन् 1918-19 की घटना है। रूस में कम्युनिस्ट क्रान्ति हो चुकी थी। जारशाही के स्तम्भ एक-एक कर ढहते जा रहे थे और लोग जो निरीह गरीब तबके का निर्ममता के साथ शोषण करते रहे थे, एक-एक कर भाग रहे थे अपने बचाव के लिए। ऐसे ही भागने वाले व्यक्तियों में एक था करेलिया प्रदेश का जागीरदार इवान। वह अपनी पत्नी अन्ना, बेटी काल्या और पुत्र कोल्या के साथ करेलिया के बीहड़ प्रदेश में नदी के तट पर भागते हुए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे।
सेण्ट पीटर्स वर्ग से कुछ मील दूर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी एक काटेज में उन्होंने शरण ली। उन लोगों के साथ उनका एक पुराना सेवक बूढ़ा मल्लाह भी था। इवान ने अपनी वासना-पूर्ति के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ अनाचार किया था, उनमें से कइयों ने तो आत्महत्या कर ली थी, अनेक अबोध बालिकायें इस क्रूर कर्म को सहन न कर पाने के कारण मर गयीं। यही हाल अन्ना का था, अपने चरित्र पर परदा पड़ा रहे इसलिए उसने अपने बाप और भाई तक को मरवा डाला था।
इसके अलावा भी जागीरदार ने हजारों निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था। उस काटेज में दोनों को अपने अतीत की याद आने लगी। संयोग की बात यह है कि जिस काटेज में उन्होंने शरण ली, वह काटेज कभी इवान का विलास महल रह चुका था। वहां का एक-एक पत्थर इवान के क्रूर कर्मों का साक्षी था। ये क्रूर कर्म इतने वीभत्स और भयावह रूप में याद आ रहे थे कि वे सब लोग जिन्हें उसने सताया था, प्रेत बनकर उससे बदला लेने के लिए उतारू लगने लगे। इस स्थिति में इवान ने अपनी पत्नी, बच्चों को बूढ़े मल्लाह के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में अन्ना इतनी विक्षिप्त हो उठी कि अपने कपड़े फाड़ने लगी, बाल नोंचने लगी और नदी पार करते समय नाव में से कूद पड़ी।
इवान का भी यही हाल हुआ। उसने भी आत्म प्रताड़ना या अतीत में किये गये क्रूर कर्मों की स्मृति से बुरी तरह भयभीत होकर नेवा झील में कूदकर आत्म-हत्या करली। स्मरणीय है दोनों पति-पत्नी अपनी क्रूरता के शिकार व्यक्तियों को नदी, झील में ही फेंका करते थे। शासन और सेना से भले ही वह बच गये परन्तु अपनी अन्तरात्मा में बैठे न्यायाधीश से बचना कहां सम्भव रहा? तत्त्वविदों का कथन है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है। वह चाहे तो देवता भी बन सकता है और यदि चाहे तो नरपिशाच भी। परन्तु इनके परिणामों में चुनाव जैसी कोई स्वतन्त्र नहीं है। जिन्होंने भी असुरता पकड़ी और नृशंसता अपनायी उन्हें अन्ततः उसका दण्ड भुगतना ही पड़ा। भले ही वे तत्काल अपने अहंकार को सन्तुष्ट कर सके हों पर परिणाम में उससे भी भयंकर यातना तथा अन्त में उनकी यंत्रणा दायक स्मृतियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला पाया है।
आत्मचेतना का उपयोग
प्राचीन काल में प्रकृति परमात्मा की इसी नियम व्यवस्था का लाभ उठाकर ऋषि-महर्षियों ने आत्मसत्ता की सामर्थ्य का लाभ उठाया था। आज भी उसके प्रमाण कभी कदा देखने को मिल जाते हैं। एक समय था जब आधुनिक विज्ञान और आत्मविद्या कभी भी न मिल सकने वाले दो परस्पर विरोधी बिन्दु माने जाते थे। इसी कारण विज्ञान की प्रगति के साथ आध्यात्मिक अवमानना हुई। किन्तु आधुनिक विज्ञान भी बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी स्थिति में आ गया है जब उसे यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि क्या शरीर ही आत्मा है या आत्मा की अभिव्यक्ति के लिये शरीर अपर्याप्त माध्यम नहीं? मनुष्य की मस्तिष्कीय चेतना की भौतिक परिधि और उसकी विराट् अवस्था दोनों के व्यापक अध्ययन से धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि सारे शरीर में मस्तिष्क के विद्यमान होने की तरह विराट् चेतना सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। शरीर उसका एक स्टेशन और मन्दिर मात्र है जिसमें वह अपने अंश या जीव रूप में कुछ क्षण विश्राम के लिये आता है। उसका अन्तिम लक्ष्य विभु या विराट् बनना है। इस उद्देश्य की पूर्ति न होने तक सन्तोष नहीं होता।
मनुष्य की चिंतन शक्ति, भावनाओं, संवेदनाओं को मात्र रासायनिक संवेग मानकर मनुष्य जीवन को नितान्त भौतिक मानने की भूल थोड़े से वैज्ञानिकों ने की है। अधिकांश ने या तो अत्यन्त गूढ़ कहकर निष्कर्ष निकालने का विचार ही त्याग दिया या फिर श्रद्धापूर्वक उनने यही स्वीकार किया कि मानवीय चेतना का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। वह भौतिकीय तत्त्वों का सम्मिलन मात्र नहीं, अपितु विराट् चेतना का ही अंश है। वह शरीर रूप नाम का पिंड मात्र नहीं, अनादि अनन्त गुण वाला चेतन तत्त्व है। शरीरों का इन्द्रियों का विकास उसकी इच्छानुसार, उसके संकल्प के आधार पर हुआ है।
भौतिक विज्ञान के जो पण्डित स्नायु-तन्त्र (नाड़ी मण्डल) को ही आत्मा मानते और उन्हीं से विचारों को उद्भूत हुआ मानते हैं उनमें जर्मनी के शरीर विज्ञानी डा. काल ह्वाक्ट तथा डा. टेन्डाल आदि प्रमुख हैं। अपने सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने अनेक प्रयोग शरीर पर किये। स्नायु-मण्डल की विस्तृत खोज की। उन्होंने उस गति की माप की जो शरीर में किसी अंग पर आघात के बाद उस अंग से भाव सन्देश के रूप में मन तक और मन से शरीर के किसी अंग तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क-बोध की सूक्ष्मता का भी पता लगाया तथा विद्युत आवेश देकर उन संदेशों को घटाने-बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की विचारों की उत्पत्ति को उन्होंने कहा यह मस्तिष्क की वैसी ही उपज होते हैं जैसे यकृत की पित्त। हालांकि अब तक वैज्ञानिक मस्तिष्क के गहन अन्धकार में झांककर जितना जान सके हैं वह अधिकतम 13 प्रतिशत है। मस्तिष्क के शेष 87 प्रतिशत भाग की कोई जानकारी नहीं है। इतनी कम जानकारी को पूर्णता की संज्ञा देना वैसे ही अविवेकपूर्ण कहा जायेगा।
फिर कुछ ऐसी घटनायें और प्रसंग भी आये दिन आते रहते हैं जो इस वैज्ञानिक मान्यता के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिक उन कारणों की कोई व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ इटली में गियोवानी गलान्ती नामक एक ऐसा बालक था जो रात के अंधेरे में भी पढ़ सकता था। 1928 में उसे इसी स्वास्थ्य परीक्षा के बाद अमेरिका नहीं जाने दिया गया था। पढ़ते समय मुख्य कार्य मस्तिष्क करता है और कोई भी मस्तिष्क प्रकाश के बिना पढ़ नहीं सकता, फिर इस बालक में यह क्षमता कहां से आई?
स्लाटलैण्ड में जेम्स क्रिस्टन नाम के एक बालक ने 12 वर्ष में ही अरबी, ग्रीक, यहूदी तथा फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषायें सीख ली थीं। 20 वर्ष तक वह विज्ञान की सभी भाषाओं का पण्डित हो गया था। उसके और सामान्य व्यक्ति के आहार और जीवन क्रम में जब कोई विशेष अन्तर नहीं था, तब बौद्धिक क्षमता में आकाश-पाताल जैसे अन्तर का कारण क्या हो सकता है? फ्रांस में जन्मे लुईस कार्डक 4 वर्ष की आयु के थे तभी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी तथा अन्य योरोपीय भाषायें बोल लेते थे। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि वह 6 माह की आयु में ही बाइबिल पढ़ लेते थे। 6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर कोई भी प्रोफेसर गणित, इतिहास और भूगोल में इनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जो ज्ञान और बौद्धिक क्षमतायें इतने अधिक अध्ययन और अभ्यास से विकसित हो पाती हैं और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार जिन्हें पदार्थ की परिणति होना चाहिये थीं, वह शारीरिक विकास के अभाव में ही इतने विकास तक कैसे जा पहुंचीं?
ब्लेइस पास्कल ने 12 वर्ष की आयु में ही ध्वनि-शास्त्र पर निबन्ध प्रस्तुत कर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया था। जीन फिलिप बेरोटियर को 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर आफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि दिन याद कराने की देर होती थी उस दिन की व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें भी टेप की भांति दुहरा सकते थे। जोनी नामक आस्ट्रेलियाई बालक को जब तीन वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो वह उसी दिन से 8वीं कक्षा के छात्रों की पुस्तकें पढ़ लेता था। उसे हाई स्कूल में केवल इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सका क्यों उस समय उसकी आयु कुल 5 वर्ष थी जबकि निर्धारित आयु 12 वर्ष न्यूनतम थी।
कोई भी अल्पबुद्धि व्यक्ति यह स्पष्ट समझ सकता है कि यह असामान्य ज्ञान पूर्व जन्मों के ही संस्कार हो सकते हैं। हमारे मनीषी निरन्तर स्वाध्याय की आवश्यकता अनुमोदित करते रहे और यह बताते रहे कि ज्ञान आत्मा की भूख-प्यास की तरह है। उससे उसका विकास होता है। यह बात समझ में आने वाली है कि चेतना का विकास ज्ञान साधना से ही सम्भव है जो अद्भुत क्षमता के रूप में हर किसी को मिलती है। बालकों के आहार, वातावरण, पोषण आदि की समान सुविधायें होने पर भी बौद्धिक असमानता इन्हीं भारतीय मान्यताओं की समर्थक हैं।
इटली के डा. लोम्ब्रोसो जिन्होंने एक समय एक प्रतिष्ठापना दी थी कि रचना विज्ञान की दृष्टि से एक पागल और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों में समरूपता होती है। इस बात को भौतिकवादियों ने बहुत अधिक उछाला, किन्तु वे यह भूल गये कि देखने में नमक और शक्कर दोनों में समानता दिखाई देने पर भी उनके गुणों में इतना अन्तर होता है कि एक के भाव 5 रु. किलो होते हैं तो दूसरे के 10 पैसे किलो। प्रतिभाशाली व्यक्तियों, आध्यात्मिक, धार्मिक संतों के विचारों में रचनात्मक जागरूकता और मार्गदर्शन की क्षमता होती है। उन्होंने सैकड़ों लोगों के जीवन में शांति, सुरुचि और सुव्यवस्था दी जबकि पागल के विचार अस्त व्यस्त होते हैं। उसे लोग दुत्कारते ही हैं, उसकी सुनता कोई नहीं।
लोम्ब्रोसी के उक्त प्रतिपादन का खण्डन अनेक वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। डा. मोर्शले ने उपरोक्त मत से असहमति व्यक्त की है और लिखा है कि सामान्य मस्तिष्क में दुनियादारी की प्रवृत्ति तो होती है, किन्तु सूक्ष्म चिन्तनशक्ति असाधारण लोगों में ही होती है।
मैडम ब्लैवटस्की का कथन है कि मस्तिष्क उस वीणा व वायलिन की तरह है जिसके तार को जितना अधिक खींचा व कसा जायेगा ध्वनि कम्पन उतने ही सूक्ष्म और मोहक होंगे। असामान्य मस्तिष्क की असामान्य उपलब्धियां ऐसी ही हैं तार कसने में उसके टूटने का भय होता है। इसलिए उसे धीरे-धीरे सावधानी से कसते हैं। मस्तिष्क को जिन साधनों (योग विद्या) से सूक्ष्म तत्वग्राही और संवेदनशील बनाया जाता है उनकी भी यही प्रवृत्ति होती है। एकाएक कठोर अभ्यास—पागल और विक्षिप्त कर भी सकते हैं, इसलिए साधना का क्रम मार्ग-दर्शकों की देख-रेख में धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। शारीरिक अभ्यास, उपवास आदि से शरीर शोधन, विचारों में प्रकाश अवधारणा आदि से ही उच्च क्षमताएं विकसित होती हैं। योगियों पर कोई स्नायविक दबाव नहीं पड़ता, कोई बीमारी नहीं होती। अतएव सूक्ष्म विचारों की महत्त्व के साथ-साथ योग-साधनाओं की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। चिंतन के सूक्ष्मतर होने से ज्ञान चेतना के कोश परस्पर जुड़ते हुए चले जाते हैं और सामान्य मस्तिष्क जो सन्देश, प्रेरणायें, अनुभूतियां नहीं गृहण कर पाते उनके लिए सुलभ हो जाती हैं। सर आलिवर लाज ने भी अपनी बौद्धिक क्षमतायें इसी आधार पर विकसित की थीं और यह माना था कि हमारी ज्ञान चेतना पदार्थ जन्य न होकर विराट् चेतना का ही एक अंश और अंग है। जब तक इस बात को नहीं समझते तब तक हमारे दृष्टिकोण भी भौतिकतावादी बने रहते हैं। तब पाप-पुण्य में कोई अन्तर ही नहीं रहता, नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं होता। आज जो सर्वत्र पीड़ा और पतन के दृश्य हैं, स्वार्थ संकीर्णता ने पुण्य-परमार्थ को दबोच रखा है, वह उसी मान्यता का दुष्परिणाम है।
पूर्वी मनोविज्ञान या भारतीय दर्शन के पीछे शोधों की एक लम्बी विज्ञान सम्मत श्रृंखला है जबकि पश्चिमी मनोविज्ञान अभी 30-40 वर्ष का बालक मात्र है जो सतह पर खड़ा स्नान करता है। उसमें इतनी क्षमता भी नहीं कि गहरे जाकर गोता लगा सके। इसीलिए वह जितने समाधान प्रस्तुत करता है उतने ही प्रश्न और समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। ऊपर मस्तिष्क की जिन अदम्य क्षमताओं का वर्णन किया गया है उन्हें कुछ देर के लिये भूल भी जायें तो भी जब मस्तिष्क सामान्य नहीं होता तब भी चेतन क्रियायें चलती रहती हैं। न केवल जागृत अवस्था में अपितु स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था में भी चेतना बनी रहती है उसका भी समाधान आवश्यक है। डा. ड्यूप्रेल ने अपनी पुस्तकों में ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिनसे यह सिद्ध होता है कि समय या अनुभूति के एक सेकेंड के करोड़वें भाग में ही महाकाल या अनेक वर्षों में हुए ज्ञान की अनुभूति कैसे सम्भव हो जाती है। इसका अर्थ तो स्पष्टतः यही होता है कि कोई एक ऐसी चेतना है जो विराट् है और उसके लघुत्तम अंश में भी वही सम्भावनायें सन्निहित हैं। अपनी पुस्तक में डा. प्रेल ने एक व्यक्ति के स्वप्न का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस व्यक्ति की गर्दन का एक उंगली से स्पर्श किया गया। उसकी नींद टूट गई। जब उससे अनुभव के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने स्वप्न देखा कि मैंने किसी की हत्या करदी, उस व्यक्ति के घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने पकड़ा, जेल भेजा, मुकदमा चला, वकील की जिरह हुई, मुझे फांसी की सजा हो गई। नियम समय पर जल्लाद आया, उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और नींद टूट गई।
डा. प्रेल लिखते हैं जिस तरह ज्ञान के अंश में ही विराट्-काल व्याप्त होने का यह उदाहरण है उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात है सम्मोहन की अवस्था में (हिप्नोटिज्म) व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसे अपनी स्थिति का भी बोध नहीं रहता, आंखें देख नहीं सकतीं, कान सुन नहीं सकते, पलकें तीव्र विद्युत प्रकाश में भी सिकुड़ती हैं, त्वचा स्पर्श ज्ञान से शून्य हो जाती है। हृदय की धड़कन बन्द-सी हो जाती है, अत्यन्त संवेदनशील यंत्रों से ही जीवन का बोध होता है। कार्बन तत्त्व अत्यधिक बढ़ जाने से मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो जाना चाहिए था। जड़ता, अगति या मृत्यु हो जानी चाहिए थी किन्तु तब ज्ञान की क्षमतायें जागृति से भी अनेक गुनी अधिक बढ़ जाती हैं। अर्थात् सम्मोहन की अवस्था में बाल्यावस्था की जो घटनायें याद नहीं रहतीं वे भी स्मरण शक्ति में आ जाती है। सामान्य स्थिति में कोई पुस्तक का एक पैराग्राफ पढ़े तो तीव्र बुद्धि व्यक्ति ही उसके कुछ शब्द दोहरा सकते हैं पर सम्मोहित अवस्था में तो यदि भाषा उसकी पढ़ी हुई नहीं तो भी अक्षर-ब-अक्षर दोहरा सकता है। जागृत अवस्था में आंख की शक्ति सीमित होती है, किन्तु उस स्थिति में कमरे में बन्द रहकर भी सैकड़ों मील दूर की वस्तुएं तक दिखाई देती हैं यह सब कैसे सम्भव है? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्म-चेतना विराट् चेतना का ही अंश है जिसमें असीम ज्ञान की शक्ति, अद्वितीय क्षमताओं की सम्भावना सन्निहित है। भूत, भविष्य और वर्तमान उसी में अवस्थित हैं, वह पदार्थ से परे है तथा उसे जानने में ही जीवन की सार्थकता है। योग-साधना, ध्यान-धारणा और-साधन अभ्यासों द्वारा इन्हीं शक्ति-केन्द्रों को जागृत किया जाता है तथा दिव्य-शक्ति सम्पन्न हुआ जाता है।