युगगीता (भाग-३) 
‘महावाक्य’ से समापन होता है, कर्म संन्यास योग की व्याख्या का
Read Scan Version
महावाक्य एवं उसकी व्याख्या
श्री भगवान् इस अंतिम श्लोक में जो कह रहे हैं वह भलीभाँति समझने योग्य है। दो पंक्तियों में मानो वेदव्यास ने श्रीकृष्ण के सारे प्रतिपादन को समाहित कर दिया है। कर्मयोग की महत्ता बताते- बताते भगवान् सारी साधनाओं की सिद्धि का मर्म भी कह जाते हैं। वह मर्म है- ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर संपूर्ण समर्पण। भगवान् को तत्त्व से जानना। अपने सभी यज्ञीय कर्मों एवं तप- साधनादि कठोर संयम से पाले गए व्रतों का भोक्ता प्रभु को मानना, स्वयं को नहीं। ईश्वर को स्वार्थरहित, पक्षपात रहित एवं दयालु मानकर उसके प्रति पूरे निष्ठाभाव से समर्पण। वह सुहृद है, दयालु है, प्रेमी है, यह मानकर निष्काम भाव से अपने सभी कर्म एवं आत्मिक प्रगति के लिए किए गए साधना- उपचार करते चलना। कभी फल की कामना में जल्दबाजी न करना। यह गीता के योग की पराकाष्ठा है, जिसमें प्रभु इस महावाक्य के माध्यम से परमशांति की मानो कुंजी अर्जुन के माध्यम से हमें सौंप देते हैं।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ ५/२९
यह जो अंतिम श्लोक है पाँचवें अध्याय का, सभी साधकों के लिए जो कर्म-संन्यासयोग जानना चाहते हैं, एक प्रकार से सूत्र रूप में की गई समग्र व्याख्या है। कर्मयोग में ज्ञान व भक्ति का स्थान-स्थान पर तालमेलपूर्वक समन्वय एवं जीवन को सर्वांगपूर्ण ढंग से जीवन का विज्ञान गीता की विशेषता है। गीता जीवन प्रबंधन की पाठ्य पुस्तिका है एवं स्थान-स्थान पर योगत्रयी को जीवन में समाहित करने का संदेश देती रहती है। मानव की सबसे बड़ी इच्छा इस लोक में शांति पाने की है। वह परमात्म-तत्त्व को जाने बिना संभव नहीं। परमात्मा को कर्म से समझकर कर्मयोग का भलीभाँति संपादन कर तथा इस परमपिता परमात्मा को सर्वलोक महेश्वर मानकर सर्वतोभावेन समर्पण-यही वह राजमार्ग है, जिस पर चलकर मनुष्य को शांति मिल सकती है। तनावमुक्त जीवन, आत्मिक प्रगति का खुले वातायनों से भरा पथ इस प्रक्रिया से सुलभ हो जाता है।
सर्वलोक महेश्वर को अर्पण
चूँकि परमात्मा ही सभी प्रकार के यज्ञों एवं तपों के भोक्ता हैं, इसलिए मुक्ति की कामना रखने वाले सभी साधकों को अपने सभी कर्मों को यज्ञ व तप रूप में करते हुए विराट् पुरुष उस महेश्वर को उनके फल को अर्पित कर देना चाहिए। मुक्त पुरुष यदि बंधनों से मुक्त भी हो गया है, तो भी उसे लोकसंग्रह हेतु (लोकशिक्षण हेतु) कर्म करते रहना चाहिए अर्थात् भटकों को राह दिखाने, सन्मार्ग के पथ पर चलने का शिक्षण देते रहना चाहिए। छब्बीसवें श्लोक में भगवान् ने एक शब्द का प्रयोग किया है-‘‘अभितो वर्तते’’। निर्वाण केवल अंदर ही नहीं, हमारे चारों ओर भी विद्यमान हो। हम उस ब्रह्मचैतन्य में निवास करें। यही बात इस अंतिम श्लोक में बताई है कि वही मुनि है, जिसने अपने अंदर , अपने चारों ओर निर्वाण लाभ प्राप्त कर लिया है, फिर भी वह जीवमात्र के कल्याण में सतत निरत रहता है। जो भगवान् के साथ उन्हें तत्त्व से जानकर एक रूप हो गया, वह मनुष्य मात्र से दिव्य प्रेम कर सकता है। ईश्वर को दयालु, प्रेमी मानने के बाद व्यक्ति उस विराट् पुरुष का ही एक अंग बन जाता है एवं एक प्रकार से उनके कर्म को तत्त्व से जानकर शांति की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है।
अंतिम श्लोक रूपी महावाक्य-आखिरी वचन से जो हम कर्म समझ पाते हैं, वह हमारे जीवन के हर क्षण में उतर जाए, तो हम एक सच्चे दिव्यकर्मी बन सकते हैं। ऐसे महामानव को कर्म करते हुए जो दिव्य शांति मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अंतिम श्लोक में जो ‘‘सर्वलोकमहेश्वर’’ शब्द आया है, उसे कई बार हम कर्मरूप में समझ नहीं पाते। इसे समझाते हुए श्री जयदयाल गोयंदका जी अपनी तत्त्वविवेचिनी टीका में लिखते हैं कि अपने-अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने ईश्वर हैं, भगवान् उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर-परमेश्वर हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद् का हवाला देते हुए वे कहते हैं, ‘‘तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्’’ (उन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को) पद इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस रूप में भगवान् को मानने वाला भक्त कभी भटकता नहीं। काम-क्रोधादि विकार उसके पास कभी फटकते नहीं। ऐसा भक्त शांत, निर्विकार एवं सदैव प्रभु के ध्यान में डूबा रहता है।
भगवान् को अहैतुक प्रेमी मान लेना व यह विश्वास करना कि वे जो भी कुछ करते हैं, मेरे मंगल के लिए करते हैं, इस श्लोक की धुरी है। लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाते, इसीलिए दुःखी बने रहते हैं व कभी शांति को प्राप्त नहीं होते। यदि सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता व सर्वदर्शी परमात्मा हमें अपना सुहृद मानता है और हम भी इस तथ्य पर विश्वास कर उसे अपना सखा, प्रेमी, निःस्वार्थ भाव से साथ दे रहा सहयोगी मान लें तो हम अलौकिक आनंद प्राप्त करेंगे एवं अपूर्व शांति को हस्तगत करेंगे।भगवान् को तीन गुणों से पहचानें
ऊपर तीन बातें बताई गई। भगवान् को यज्ञों व तपों का भोक्ता मानना, समस्त लोकों का महेश्वर मानना तथा सभी प्राणियों को सुहृद मानना। यदि इन तीन में से साधक-योगी किसी एक पर भी अडिग रह दृढ़ विश्वास कर ले, तो वह परमशांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक दिव्यकर्मी वह ही है, जो इन तीनों के अर्थ को भलीभाँति समझकर किसी एक पर या तीनों पर दृढ़ विश्वास रख महापुरुषों के सत्संग, मनन, श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय द्वारा श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अपनी जीवनयात्रा को आगे बढ़ाए। उसका इहलोक-परलोक दोनों ही सध जाएँगे।
परमपूज्य गुरुदेव ने अपने जीवनकाल के पूर्वार्द्ध में सबसे पहली पुस्तक लिखी-‘‘मैं क्या हूँ’’। वेदांत दर्शन पर आधारित यह पुस्तक एक आत्मनिवेदन रूप में यह बताती है कि हमारे अंदर विद्यमान आत्मसत्ता में कितनी शक्ति भरी पड़ी है। वह किस विराट् सत्ता की अंशधारी है। बाद में पूज्यवर ने काफी पुस्तकें लिखीं, परंतु ‘ईश्वर और उसकी अनुभूति’, ‘ईश्वर कौन है? कहाँ है? कैसा है? तथा ‘आत्मज्ञान जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि’ इस विषय पर सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। इन पुस्तकों में वही व्याख्या है, जो गीता के पाँचवें अध्याय के इस २९वें श्लोक में वर्णित है। ईश्वर को जान-समझ लिया, तो फिर सारे क्लेशों, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। परमपूज्य गुरुदेव इस संबंध में ईसा एवं रामकृष्ण परमहंस से संबंधित उस घटना का उल्लेख करते थे, जिसमें कुष्ठग्रस्त रोगी की सेवा ईश्वर मानकर की गई थी। किसी भी प्रकार की जुगुप्सा नहीं, कोई और भाव नहीं। जीवमात्र में जब ईश्वर की झलक दिखाई देती है, तो मनुष्य ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ का भाव रख सेवा प्रधान जीवन जीने लगता है।
पूरे अध्याय का सारामृत
छठवें अध्याय की ओर बढ़ने से पूर्व इस महत्त्वपूर्ण पाँचवें अध्याय के सारामृत को एक बार फिर ग्रहण करने का प्रयास करें, ताकि तेरह माह से चला आ रहा यह स्वाध्याय जड़ जमाकर हमारे अंतस् में बैठ जाए एवं हमारे कर्मों में उतरने लगे। इस अध्याय का शुभारंभ ही अर्जुन की जिज्ञासा से हुआ है। वह भ्रमित है। उसने चौथे अध्याय में कर्मयोग की महिमा जानी, किंतु बीच-बीच में श्रीकृष्ण के श्रीमुख से ज्ञानयोग (कर्म संन्यास) की बातें भी ‘ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति’ (श्लोक २५ ) तथा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि....’ (श्लोक २४) के माध्यम से जानीं। श्रीकृष्ण से अर्जुन यह जानना चाहता है कि कौन-सा साधन श्रेष्ठ है—कर्मयोग अथवा ज्ञानयोग।
भगवान् ने अर्जुन को यहाँ बताया है कि पूर्णतया कर्मफल का परित्याग कर वह कर्मयोगी, नित्य संन्यासी बने। गीता का उपदेश कर्म त्यागना नहीं है, न ही स्वधर्म त्यागना। कर्म त्याग करके संसार में रहना संभव नहीं है। मनुष्य दिव्यकर्मी बने, न किसी से द्वेष करे, न किसी वस्तु की आकांक्षा रखे। राग-द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति संन्यासी के ही समान है, यह श्रीकृष्ण का प्रतिपादन है। आगे वे ज्ञानियों व नासमझों में अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि पंडितजन (ज्ञानी-अध्यात्म के मर्म को समझने वाले) जानते हैं कि कर्म-संन्यास एवं कर्मयोग दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं- परमात्मा की ओर। उन्हें पृथक् फल देने वाला नहीं मानना चाहिए। दोनों ही मार्ग पर चलकर मनुष्य परमात्मा के परमधाम तक पहुँचता है। आगे वे कहते हैं कि यदि कोई दिव्यकर्मी कर्म करते हुए जीवन व्यापार में सामान्य क्रम से जीते हुए अपने मन को अपने वश में रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है एवं अंतःकरण को शुद्ध बनाए रखता है, सभी प्राणियों में परमात्मा की झाँकी देखता है, तो वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। हर कर्मयोगी को ज्ञानयोग के इस मर्म को मन में बिठाकर भगवत्स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यहाँ प्रभु, जो योगेश्वर भी हैं एवं नीतिपुरुष भी, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के एक सम्यक् संतुलन को जीवन में उतारने का शिक्षण देते हैं। (श्लोक ६ व ७)जीवन जीने की कला के ये कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्र हैं।
आसक्ति को त्यागो
शिष्य अर्जुन के गुरु श्रीकृष्ण उसे बताते हैं कि उसे ऐसा कर्मयोगी बनना चाहिए जो काया, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से मात्र प्रभु अर्पित होकर कर्म करता है। वह समाज-समष्टि के हित हेतु जीवन जीता है एवं ये दिव्यकर्म मात्र अपनी अंतःशुद्धि हेतु करता है (श्लोक ११)। श्रीकृष्ण बार-बार एक बात पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देते हैं-‘संगंत्यक्त्वा’ अर्थात् आसक्तियों को छोड़कर कर्म करो। (ऐसे आसक्तिरहित जीवन जीने वाले दिव्यकर्मी जैसे बालगंगाधर तिलक एवं हमारे गुरुदेव पं० श्रीराम शर्मा आचार्य जी) इस प्रकार से किए गए कर्मों की परिणति बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि इससे कर्मयोगी भगवत् प्राप्तिरूपी शांति को प्राप्त होता है। सकाम कर्म करने वाला तो बंधनों में फँसता चला जाता है (श्लोक १२)।
आगे श्रीकृष्ण कर्मयोग से अर्जुन का ध्यान ज्ञानयोग की ओर आकर्षित करते हैं कि परमेश्वर तो कर्मफल संयोग से परे हैं, यह तो मानवी प्रकृति है, जो उससे कर्म करा रही है। यदि अज्ञान से ढके हुए ज्ञान के अमृतकण ग्रहण कर लिए जाएँ, तो उस दुर्गति से बचा जा सकता है, जो आज के आम आदमी की हो रही है। वह तो अज्ञान से मोहित हो, शिश्रोदरपरायण जीवन जी रहा है। परमात्मा का तत्त्वज्ञान उस अज्ञान को नष्ट कर देता है, जो सद्ज्ञानरूपी सूर्य पर बदली बनकर छाया हुआ है अथवा शीशे पर मैल की परत के रूप में विद्यमान है। (श्लोक १५,१६) अब श्रीकृष्ण भक्तियोग की सीढ़ी पर अर्जुन को चढ़ाते हैं व कहते हैं कि अपनी मन-बुद्धि को वह परमात्मा में विलय कर दे, अपनी निष्ठा आदर्शों के समुच्चय परमात्मा में रखे तथा तत्परायण (उन्हीं परब्रह्म परमात्मा में एकीभाव से स्थित) बनने की कोशिश करे। ऐसा करने पर वह परमगति को प्राप्त होगा, बार-बार वासनाओं के वशीभूत हो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ‘ज्ञान निर्धूत कल्मषाः’ को उद्धृत कर वे कहते हैं कि ज्ञान द्वारा पापरहित होने पर योगी के हर कर्म दिव्यकर्म बन जाते हैं (श्लोक १७)।
ब्रह्मणि स्थितः
बड़ी विलक्षण है—इस अध्याय के उनतीस श्लोकों की यात्रा। एक-एक श्लोक मानो एक अध्याय के समान है। तुरंत अगले श्लोक में योगेश्वर कह बैठते हैं कि जो योगी अपनी भाँति संपूर्ण भूतों में-जीवधारियों में, गौ, हाथी, कुत्ते अथवा चांडाल, ब्राह्मण में सभी को समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठतम योगी है एवं सही मायने में ज्ञानी है (श्लोक १८)। आगे छठे अध्याय के ३२वें श्लोक में भी कुछ ऐसा ही प्रतिपादन हम सुनेंगे। समभाव में स्थित योगी ऐसे जीता है, मानो उसने सारा संसार जीत लिया हो। वह सदैव ब्रह्म में स्थित होकर कर्म करता है। कौन-सा योगी ब्रह्म में स्थित हो सकता है, इसके लिए श्रीकृष्ण कुछ विशेषताएँ भी बताते हैं-जो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्र न हो, सदैव कर्म करता रहे एवं अपनी बुद्धि को प्रभु के श्री चरणों में नियोजित कर समर्पित भाव से जिए (श्लोक १९,२०)।
आगे श्रीकृष्ण अक्षय आनंद की प्राप्ति का सूत्र अर्जुन को बताते हैं। आदिकाल से मानव को इसी की तो तलाश रही है। दुर्भाग्यवश वह उसे इंद्रिय सुख में खोजता है। वहाँ से आसक्ति हटे, अंतर्मुखी हो वह ध्यानरूपी योग द्वारा सच्चिदानंदघन परब्रह्म परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करे, तो ही उसे वह आनंद मिलेगा। बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसी कारण बहिरंग के भोग को छोड़कर अंतः के ब्रह्म में रमण करता है। (श्लोक २१,२२) सच्चे सुख की, अनिर्वचनीय आनंद एवं अक्षय शांति की यही कुंजी है। शरीर हमारा भोगों में नष्ट हो-दुःख के हेतु बने विषयों में लिप्त हो जर्जर बन जाए, उसके पूर्व ही हमारा विवेक जाग जाना चाहिए एवं हमें काम-क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने हेतु स्वयं को समर्थ बना लेना चाहिए। काम और क्रोध परस्पर जुड़े हैं। दमित काम ही क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है तथा क्रोध आदमी की सारी शक्ति को नष्ट कर डालता है। जो इन दोनों आवेगों को नियंत्रित कर ले, श्रीकृष्ण की दृष्टि में वही योगी है, वही सुखी है-(स युक्तः स सुखी नरः) (श्लोक २३)।
शांत परब्रह्म बने हमारा इष्ट
तो फिर कर्मयोगी को, जो ज्ञानी भी है एवं तत्परायण एक भक्त भी, क्या करना चाहिए। उसे ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। आत्मा में ही रमण कर, आत्मज्ञान को प्राप्त कर, अपने सभी पापों व संशयों को नष्ट कर सर्वहितार्थाय कर्म करने वाला योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह शांत परब्रह्म ही हम सबका इष्ट है। ऐसे व्यक्ति अपने अंदर व अपने आस-पास भी शांति का वातावरण बना देते हैं। ये युग प्रवर्तक होते हैं। युगनायक होते हैं एवं दूसरों के लिए जीते हैं। काम-क्रोधरूपी विकारों से ये मुक्त होते हैं तथा अपने चित्त पर, स्वभावजन्य आदतों पर इनका अपना नियंत्रण होता है। ऐसे व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा की चेतना से आपूरित होते हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके होते हैं (श्लोक २४,२५)। हर व्यक्ति के अंदर ऐसे दिव्ययोगी बनने की अनंत संभावनाएँ मौजूद हैं।
प्रतिपादन की पराकाष्ठा
अब अंतिम तीन श्लोकों में श्रीकृष्ण ऐसे दिव्य योगी बनने की प्रक्रिया की एक झलक दिखाकर अपने इस कर्म-संन्यास योग नामक प्रकरण वाले अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। जैसे फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, कंप्यूटर के पॉवर पाइंट द्वारा गहन विषय को सूत्र रूप में समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक उसी तरह सत्ताईसवें, अट्ठाईसवें श्लोक में ध्यान की विधि एवं मोक्षप्राप्ति (जीवनमुक्ति-बंधनमुक्ति) कैसे की जाए, इसकी एक झलक दिखा दी गई है। इसका विस्तार छठे अध्याय में है; परंतु पहले श्लोक में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले अर्जुन की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर श्रीकृष्ण अपनी पराकाष्ठा पर उनतीसवें श्लोक में पहुँचते हैं, जहाँ वे अपने भक्त की परिभाषा बताते हैं-अपनी विशेषताएँ बताते हैं व भगवत्प्राप्ति से ही शांति मिलती है, यह समझाते हैं। यहीं पाँचवाँ अध्याय समाप्त हो जाता है पर व्याख्या का क्रम जारी है क्यों कि ध्यान योग की पूर्व भूमिका बन चुकी है। वह अगले छठें अध्याय में भी जारी रहती है। किंतु यहाँ पाँचवे अध्याय का समापन करते हैं।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥५॥
श्री भगवान् इस अंतिम श्लोक में जो कह रहे हैं वह भलीभाँति समझने योग्य है। दो पंक्तियों में मानो वेदव्यास ने श्रीकृष्ण के सारे प्रतिपादन को समाहित कर दिया है। कर्मयोग की महत्ता बताते- बताते भगवान् सारी साधनाओं की सिद्धि का मर्म भी कह जाते हैं। वह मर्म है- ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर संपूर्ण समर्पण। भगवान् को तत्त्व से जानना। अपने सभी यज्ञीय कर्मों एवं तप- साधनादि कठोर संयम से पाले गए व्रतों का भोक्ता प्रभु को मानना, स्वयं को नहीं। ईश्वर को स्वार्थरहित, पक्षपात रहित एवं दयालु मानकर उसके प्रति पूरे निष्ठाभाव से समर्पण। वह सुहृद है, दयालु है, प्रेमी है, यह मानकर निष्काम भाव से अपने सभी कर्म एवं आत्मिक प्रगति के लिए किए गए साधना- उपचार करते चलना। कभी फल की कामना में जल्दबाजी न करना। यह गीता के योग की पराकाष्ठा है, जिसमें प्रभु इस महावाक्य के माध्यम से परमशांति की मानो कुंजी अर्जुन के माध्यम से हमें सौंप देते हैं।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ ५/२९
यह जो अंतिम श्लोक है पाँचवें अध्याय का, सभी साधकों के लिए जो कर्म-संन्यासयोग जानना चाहते हैं, एक प्रकार से सूत्र रूप में की गई समग्र व्याख्या है। कर्मयोग में ज्ञान व भक्ति का स्थान-स्थान पर तालमेलपूर्वक समन्वय एवं जीवन को सर्वांगपूर्ण ढंग से जीवन का विज्ञान गीता की विशेषता है। गीता जीवन प्रबंधन की पाठ्य पुस्तिका है एवं स्थान-स्थान पर योगत्रयी को जीवन में समाहित करने का संदेश देती रहती है। मानव की सबसे बड़ी इच्छा इस लोक में शांति पाने की है। वह परमात्म-तत्त्व को जाने बिना संभव नहीं। परमात्मा को कर्म से समझकर कर्मयोग का भलीभाँति संपादन कर तथा इस परमपिता परमात्मा को सर्वलोक महेश्वर मानकर सर्वतोभावेन समर्पण-यही वह राजमार्ग है, जिस पर चलकर मनुष्य को शांति मिल सकती है। तनावमुक्त जीवन, आत्मिक प्रगति का खुले वातायनों से भरा पथ इस प्रक्रिया से सुलभ हो जाता है।
सर्वलोक महेश्वर को अर्पण
चूँकि परमात्मा ही सभी प्रकार के यज्ञों एवं तपों के भोक्ता हैं, इसलिए मुक्ति की कामना रखने वाले सभी साधकों को अपने सभी कर्मों को यज्ञ व तप रूप में करते हुए विराट् पुरुष उस महेश्वर को उनके फल को अर्पित कर देना चाहिए। मुक्त पुरुष यदि बंधनों से मुक्त भी हो गया है, तो भी उसे लोकसंग्रह हेतु (लोकशिक्षण हेतु) कर्म करते रहना चाहिए अर्थात् भटकों को राह दिखाने, सन्मार्ग के पथ पर चलने का शिक्षण देते रहना चाहिए। छब्बीसवें श्लोक में भगवान् ने एक शब्द का प्रयोग किया है-‘‘अभितो वर्तते’’। निर्वाण केवल अंदर ही नहीं, हमारे चारों ओर भी विद्यमान हो। हम उस ब्रह्मचैतन्य में निवास करें। यही बात इस अंतिम श्लोक में बताई है कि वही मुनि है, जिसने अपने अंदर , अपने चारों ओर निर्वाण लाभ प्राप्त कर लिया है, फिर भी वह जीवमात्र के कल्याण में सतत निरत रहता है। जो भगवान् के साथ उन्हें तत्त्व से जानकर एक रूप हो गया, वह मनुष्य मात्र से दिव्य प्रेम कर सकता है। ईश्वर को दयालु, प्रेमी मानने के बाद व्यक्ति उस विराट् पुरुष का ही एक अंग बन जाता है एवं एक प्रकार से उनके कर्म को तत्त्व से जानकर शांति की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है।
अंतिम श्लोक रूपी महावाक्य-आखिरी वचन से जो हम कर्म समझ पाते हैं, वह हमारे जीवन के हर क्षण में उतर जाए, तो हम एक सच्चे दिव्यकर्मी बन सकते हैं। ऐसे महामानव को कर्म करते हुए जो दिव्य शांति मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अंतिम श्लोक में जो ‘‘सर्वलोकमहेश्वर’’ शब्द आया है, उसे कई बार हम कर्मरूप में समझ नहीं पाते। इसे समझाते हुए श्री जयदयाल गोयंदका जी अपनी तत्त्वविवेचिनी टीका में लिखते हैं कि अपने-अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने ईश्वर हैं, भगवान् उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर-परमेश्वर हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद् का हवाला देते हुए वे कहते हैं, ‘‘तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्’’ (उन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को) पद इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस रूप में भगवान् को मानने वाला भक्त कभी भटकता नहीं। काम-क्रोधादि विकार उसके पास कभी फटकते नहीं। ऐसा भक्त शांत, निर्विकार एवं सदैव प्रभु के ध्यान में डूबा रहता है।
भगवान् को अहैतुक प्रेमी मान लेना व यह विश्वास करना कि वे जो भी कुछ करते हैं, मेरे मंगल के लिए करते हैं, इस श्लोक की धुरी है। लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाते, इसीलिए दुःखी बने रहते हैं व कभी शांति को प्राप्त नहीं होते। यदि सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता व सर्वदर्शी परमात्मा हमें अपना सुहृद मानता है और हम भी इस तथ्य पर विश्वास कर उसे अपना सखा, प्रेमी, निःस्वार्थ भाव से साथ दे रहा सहयोगी मान लें तो हम अलौकिक आनंद प्राप्त करेंगे एवं अपूर्व शांति को हस्तगत करेंगे।भगवान् को तीन गुणों से पहचानें
ऊपर तीन बातें बताई गई। भगवान् को यज्ञों व तपों का भोक्ता मानना, समस्त लोकों का महेश्वर मानना तथा सभी प्राणियों को सुहृद मानना। यदि इन तीन में से साधक-योगी किसी एक पर भी अडिग रह दृढ़ विश्वास कर ले, तो वह परमशांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक दिव्यकर्मी वह ही है, जो इन तीनों के अर्थ को भलीभाँति समझकर किसी एक पर या तीनों पर दृढ़ विश्वास रख महापुरुषों के सत्संग, मनन, श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय द्वारा श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अपनी जीवनयात्रा को आगे बढ़ाए। उसका इहलोक-परलोक दोनों ही सध जाएँगे।
परमपूज्य गुरुदेव ने अपने जीवनकाल के पूर्वार्द्ध में सबसे पहली पुस्तक लिखी-‘‘मैं क्या हूँ’’। वेदांत दर्शन पर आधारित यह पुस्तक एक आत्मनिवेदन रूप में यह बताती है कि हमारे अंदर विद्यमान आत्मसत्ता में कितनी शक्ति भरी पड़ी है। वह किस विराट् सत्ता की अंशधारी है। बाद में पूज्यवर ने काफी पुस्तकें लिखीं, परंतु ‘ईश्वर और उसकी अनुभूति’, ‘ईश्वर कौन है? कहाँ है? कैसा है? तथा ‘आत्मज्ञान जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि’ इस विषय पर सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। इन पुस्तकों में वही व्याख्या है, जो गीता के पाँचवें अध्याय के इस २९वें श्लोक में वर्णित है। ईश्वर को जान-समझ लिया, तो फिर सारे क्लेशों, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। परमपूज्य गुरुदेव इस संबंध में ईसा एवं रामकृष्ण परमहंस से संबंधित उस घटना का उल्लेख करते थे, जिसमें कुष्ठग्रस्त रोगी की सेवा ईश्वर मानकर की गई थी। किसी भी प्रकार की जुगुप्सा नहीं, कोई और भाव नहीं। जीवमात्र में जब ईश्वर की झलक दिखाई देती है, तो मनुष्य ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ का भाव रख सेवा प्रधान जीवन जीने लगता है।
पूरे अध्याय का सारामृत
छठवें अध्याय की ओर बढ़ने से पूर्व इस महत्त्वपूर्ण पाँचवें अध्याय के सारामृत को एक बार फिर ग्रहण करने का प्रयास करें, ताकि तेरह माह से चला आ रहा यह स्वाध्याय जड़ जमाकर हमारे अंतस् में बैठ जाए एवं हमारे कर्मों में उतरने लगे। इस अध्याय का शुभारंभ ही अर्जुन की जिज्ञासा से हुआ है। वह भ्रमित है। उसने चौथे अध्याय में कर्मयोग की महिमा जानी, किंतु बीच-बीच में श्रीकृष्ण के श्रीमुख से ज्ञानयोग (कर्म संन्यास) की बातें भी ‘ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति’ (श्लोक २५ ) तथा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि....’ (श्लोक २४) के माध्यम से जानीं। श्रीकृष्ण से अर्जुन यह जानना चाहता है कि कौन-सा साधन श्रेष्ठ है—कर्मयोग अथवा ज्ञानयोग।
भगवान् ने अर्जुन को यहाँ बताया है कि पूर्णतया कर्मफल का परित्याग कर वह कर्मयोगी, नित्य संन्यासी बने। गीता का उपदेश कर्म त्यागना नहीं है, न ही स्वधर्म त्यागना। कर्म त्याग करके संसार में रहना संभव नहीं है। मनुष्य दिव्यकर्मी बने, न किसी से द्वेष करे, न किसी वस्तु की आकांक्षा रखे। राग-द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति संन्यासी के ही समान है, यह श्रीकृष्ण का प्रतिपादन है। आगे वे ज्ञानियों व नासमझों में अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि पंडितजन (ज्ञानी-अध्यात्म के मर्म को समझने वाले) जानते हैं कि कर्म-संन्यास एवं कर्मयोग दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं- परमात्मा की ओर। उन्हें पृथक् फल देने वाला नहीं मानना चाहिए। दोनों ही मार्ग पर चलकर मनुष्य परमात्मा के परमधाम तक पहुँचता है। आगे वे कहते हैं कि यदि कोई दिव्यकर्मी कर्म करते हुए जीवन व्यापार में सामान्य क्रम से जीते हुए अपने मन को अपने वश में रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है एवं अंतःकरण को शुद्ध बनाए रखता है, सभी प्राणियों में परमात्मा की झाँकी देखता है, तो वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। हर कर्मयोगी को ज्ञानयोग के इस मर्म को मन में बिठाकर भगवत्स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यहाँ प्रभु, जो योगेश्वर भी हैं एवं नीतिपुरुष भी, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के एक सम्यक् संतुलन को जीवन में उतारने का शिक्षण देते हैं। (श्लोक ६ व ७)जीवन जीने की कला के ये कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्र हैं।
आसक्ति को त्यागो
शिष्य अर्जुन के गुरु श्रीकृष्ण उसे बताते हैं कि उसे ऐसा कर्मयोगी बनना चाहिए जो काया, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से मात्र प्रभु अर्पित होकर कर्म करता है। वह समाज-समष्टि के हित हेतु जीवन जीता है एवं ये दिव्यकर्म मात्र अपनी अंतःशुद्धि हेतु करता है (श्लोक ११)। श्रीकृष्ण बार-बार एक बात पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देते हैं-‘संगंत्यक्त्वा’ अर्थात् आसक्तियों को छोड़कर कर्म करो। (ऐसे आसक्तिरहित जीवन जीने वाले दिव्यकर्मी जैसे बालगंगाधर तिलक एवं हमारे गुरुदेव पं० श्रीराम शर्मा आचार्य जी) इस प्रकार से किए गए कर्मों की परिणति बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि इससे कर्मयोगी भगवत् प्राप्तिरूपी शांति को प्राप्त होता है। सकाम कर्म करने वाला तो बंधनों में फँसता चला जाता है (श्लोक १२)।
आगे श्रीकृष्ण कर्मयोग से अर्जुन का ध्यान ज्ञानयोग की ओर आकर्षित करते हैं कि परमेश्वर तो कर्मफल संयोग से परे हैं, यह तो मानवी प्रकृति है, जो उससे कर्म करा रही है। यदि अज्ञान से ढके हुए ज्ञान के अमृतकण ग्रहण कर लिए जाएँ, तो उस दुर्गति से बचा जा सकता है, जो आज के आम आदमी की हो रही है। वह तो अज्ञान से मोहित हो, शिश्रोदरपरायण जीवन जी रहा है। परमात्मा का तत्त्वज्ञान उस अज्ञान को नष्ट कर देता है, जो सद्ज्ञानरूपी सूर्य पर बदली बनकर छाया हुआ है अथवा शीशे पर मैल की परत के रूप में विद्यमान है। (श्लोक १५,१६) अब श्रीकृष्ण भक्तियोग की सीढ़ी पर अर्जुन को चढ़ाते हैं व कहते हैं कि अपनी मन-बुद्धि को वह परमात्मा में विलय कर दे, अपनी निष्ठा आदर्शों के समुच्चय परमात्मा में रखे तथा तत्परायण (उन्हीं परब्रह्म परमात्मा में एकीभाव से स्थित) बनने की कोशिश करे। ऐसा करने पर वह परमगति को प्राप्त होगा, बार-बार वासनाओं के वशीभूत हो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ‘ज्ञान निर्धूत कल्मषाः’ को उद्धृत कर वे कहते हैं कि ज्ञान द्वारा पापरहित होने पर योगी के हर कर्म दिव्यकर्म बन जाते हैं (श्लोक १७)।
ब्रह्मणि स्थितः
बड़ी विलक्षण है—इस अध्याय के उनतीस श्लोकों की यात्रा। एक-एक श्लोक मानो एक अध्याय के समान है। तुरंत अगले श्लोक में योगेश्वर कह बैठते हैं कि जो योगी अपनी भाँति संपूर्ण भूतों में-जीवधारियों में, गौ, हाथी, कुत्ते अथवा चांडाल, ब्राह्मण में सभी को समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठतम योगी है एवं सही मायने में ज्ञानी है (श्लोक १८)। आगे छठे अध्याय के ३२वें श्लोक में भी कुछ ऐसा ही प्रतिपादन हम सुनेंगे। समभाव में स्थित योगी ऐसे जीता है, मानो उसने सारा संसार जीत लिया हो। वह सदैव ब्रह्म में स्थित होकर कर्म करता है। कौन-सा योगी ब्रह्म में स्थित हो सकता है, इसके लिए श्रीकृष्ण कुछ विशेषताएँ भी बताते हैं-जो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्र न हो, सदैव कर्म करता रहे एवं अपनी बुद्धि को प्रभु के श्री चरणों में नियोजित कर समर्पित भाव से जिए (श्लोक १९,२०)।
आगे श्रीकृष्ण अक्षय आनंद की प्राप्ति का सूत्र अर्जुन को बताते हैं। आदिकाल से मानव को इसी की तो तलाश रही है। दुर्भाग्यवश वह उसे इंद्रिय सुख में खोजता है। वहाँ से आसक्ति हटे, अंतर्मुखी हो वह ध्यानरूपी योग द्वारा सच्चिदानंदघन परब्रह्म परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करे, तो ही उसे वह आनंद मिलेगा। बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसी कारण बहिरंग के भोग को छोड़कर अंतः के ब्रह्म में रमण करता है। (श्लोक २१,२२) सच्चे सुख की, अनिर्वचनीय आनंद एवं अक्षय शांति की यही कुंजी है। शरीर हमारा भोगों में नष्ट हो-दुःख के हेतु बने विषयों में लिप्त हो जर्जर बन जाए, उसके पूर्व ही हमारा विवेक जाग जाना चाहिए एवं हमें काम-क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने हेतु स्वयं को समर्थ बना लेना चाहिए। काम और क्रोध परस्पर जुड़े हैं। दमित काम ही क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है तथा क्रोध आदमी की सारी शक्ति को नष्ट कर डालता है। जो इन दोनों आवेगों को नियंत्रित कर ले, श्रीकृष्ण की दृष्टि में वही योगी है, वही सुखी है-(स युक्तः स सुखी नरः) (श्लोक २३)।
शांत परब्रह्म बने हमारा इष्ट
तो फिर कर्मयोगी को, जो ज्ञानी भी है एवं तत्परायण एक भक्त भी, क्या करना चाहिए। उसे ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। आत्मा में ही रमण कर, आत्मज्ञान को प्राप्त कर, अपने सभी पापों व संशयों को नष्ट कर सर्वहितार्थाय कर्म करने वाला योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह शांत परब्रह्म ही हम सबका इष्ट है। ऐसे व्यक्ति अपने अंदर व अपने आस-पास भी शांति का वातावरण बना देते हैं। ये युग प्रवर्तक होते हैं। युगनायक होते हैं एवं दूसरों के लिए जीते हैं। काम-क्रोधरूपी विकारों से ये मुक्त होते हैं तथा अपने चित्त पर, स्वभावजन्य आदतों पर इनका अपना नियंत्रण होता है। ऐसे व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा की चेतना से आपूरित होते हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके होते हैं (श्लोक २४,२५)। हर व्यक्ति के अंदर ऐसे दिव्ययोगी बनने की अनंत संभावनाएँ मौजूद हैं।
प्रतिपादन की पराकाष्ठा
अब अंतिम तीन श्लोकों में श्रीकृष्ण ऐसे दिव्य योगी बनने की प्रक्रिया की एक झलक दिखाकर अपने इस कर्म-संन्यास योग नामक प्रकरण वाले अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। जैसे फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, कंप्यूटर के पॉवर पाइंट द्वारा गहन विषय को सूत्र रूप में समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक उसी तरह सत्ताईसवें, अट्ठाईसवें श्लोक में ध्यान की विधि एवं मोक्षप्राप्ति (जीवनमुक्ति-बंधनमुक्ति) कैसे की जाए, इसकी एक झलक दिखा दी गई है। इसका विस्तार छठे अध्याय में है; परंतु पहले श्लोक में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले अर्जुन की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर श्रीकृष्ण अपनी पराकाष्ठा पर उनतीसवें श्लोक में पहुँचते हैं, जहाँ वे अपने भक्त की परिभाषा बताते हैं-अपनी विशेषताएँ बताते हैं व भगवत्प्राप्ति से ही शांति मिलती है, यह समझाते हैं। यहीं पाँचवाँ अध्याय समाप्त हो जाता है पर व्याख्या का क्रम जारी है क्यों कि ध्यान योग की पूर्व भूमिका बन चुकी है। वह अगले छठें अध्याय में भी जारी रहती है। किंतु यहाँ पाँचवे अध्याय का समापन करते हैं।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥५॥
Versions
-
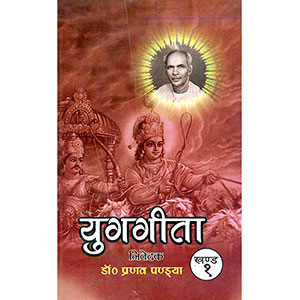
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
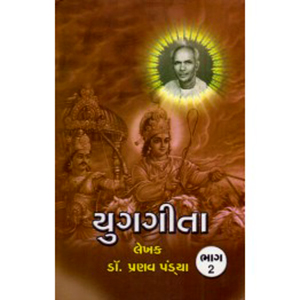
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
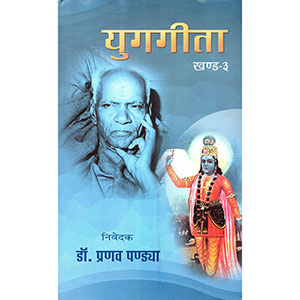
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
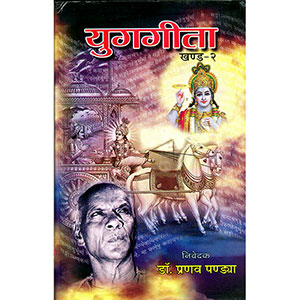
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
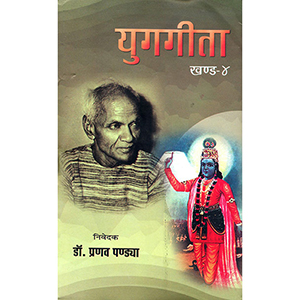
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
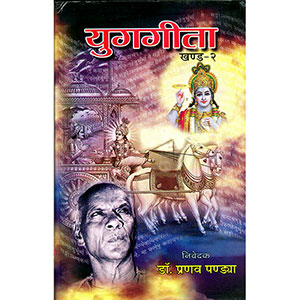
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
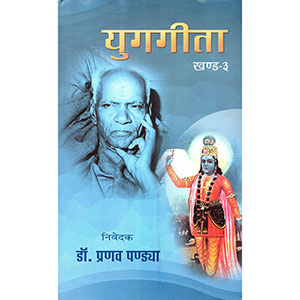
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
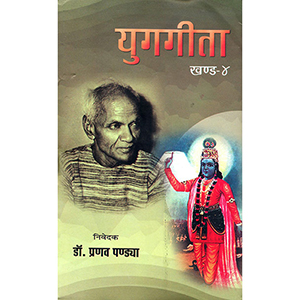
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
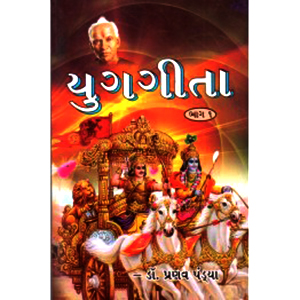
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रस्तुत तृतीय खण्ड की प्रस्तावना
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- कर्मसंन्यास एवं कर्मयोग में कौन सा श्रेष्ठ है?
- सांख्य (संन्यास) और कर्मयोग दोनों एक ही हैं, अलग-अलग नहीं
- कर्मयोग के अभ्यास बिना संन्यास सधेगा नहीं
- कर्त्ताभाव से मुक्त द्रष्टा स्तर का दिव्यकर्मी
- कर्मयोग की परमसिद्धि-अंतःशुद्धि
- न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते
- निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
- आदर्शनिष्ठ महामानव कैसे बनें
- ब्रह्म में प्रतिष्ठित संवेदनशील दिव्यकर्मी
- ज्ञानीजन क्षणिक सुखों में रमण नहीं करते
- योगेश्वर का प्रकाश-स्तंभ बनने हेतु भावभरा आमंत्रण
- परम शांतिरूपी मुक्ति का एकमात्र मार्ग
- ‘महावाक्य’ से समापन होता है, कर्म संन्यास योग की व्याख्या का
- संकल्पों से मुक्ति मिले, तो योग सधे
- योगारूढ़ होकर ही मन को शांत किया जा सकता है
- उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्
- जीता हुआ मन ही हमारा सच्चा मित्र
- कैसे बनें पूरी तरह युक्तपुरुष

