युगगीता (भाग-३) 
जीता हुआ मन ही हमारा सच्चा मित्र
Read Scan Version
मन किस प्रकार अपना ही मित्र एवं शत्रु हो सकता है, यह बात सहज
ही एक शंका के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए योगेश्वर
श्रीकृष्ण छठे श्लोक में इस बात को विस्तार से कहते हैं—
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ ६/६
इसका शब्दार्थ देखें—
जिस (येन) विवेकयुक्त बुद्धि द्वारा (आत्मना) मन ही (आत्मा एव) जीत लिया है—वशीभूत कर लिया गया है (जितः), मन (आत्मा)उसके (तस्य) जीवात्मा का (आत्मनः) मित्र है (बन्धुः, किंतु (तु) अवशीभूत व्यक्ति का (अनात्मनः) मन (आत्मा) शत्रु की तरह (शत्रुवत्) शत्रुता का आचरण करने में (शत्रुत्वे) प्रवृत्त हो जाता है (वर्तते)।
अर्थात् जिसने अपने आत्मा द्वारा अपने मन एवं इन्द्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, उसके लिए यह आत्मा मित्र है; किंतु जिसने अपने आत्मा को जीता नहीं है, उसका आत्मा ही उसका विरोधी हो जाता है और उसके प्रति बाह्य शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जीव को वह हर प्रकार की हानि पहुँचाता है। (श्लोक ६, अध्याय ६)
कितनी सुंदर उत्तरार्द्धपरक चर्चा इस श्लोक में आई है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसके लिए उसका बौद्धिक व्यक्तित्व मित्र है (बन्धुरात्मात्मनस्तस्य) और यदि हम किसी कारणवश अपने मन, इन्द्रियों, बुद्धि वाले पक्ष पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो, यह अविजित बुद्धि ही हमारे विरुद्ध एक भयावह अजेय शत्रु की तरह काम करती है। यहाँ वह अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य का अपना आपा कब मित्र हो जाता है, कब शत्रु। जिसने अपने को जीत लिया, अपनी इंद्रियों पर अपना स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसका मन उसका मित्र है। संसार की आसक्तियों से स्वयं को हटाते चलना एवं भगवान् में मन लगाते चलना, सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्वयं को सम्यक् रूप में स्थित करना ही एकमात्र बंधनमुक्ति का उपाय है।
मित्र- शत्रु हमारे अपने ही अंदर
हम स्वभाव से बहिर्मुखी हैं। अपने मित्र एवं शत्रु हम बाहर ही ढूँढ़ते रहते हैं। वस्तुतः बाहर—बहिरंग जगत् में न तो हमारा कोई मित्र है और न कोई शत्रु ही है। ये सभी हमारे भीतर अंतरंग में विद्यमान हैं। हमारा अपना अहं जो अनुशासनों के पालन की बात आने पर बाधक बनने लगता है तथा हमारे अपने बौद्धिक व्यक्तित्व- परिष्कृत आत्मतत्त्व के मार्गदर्शन में चलने से इनकार कर देता है तो यह हमारी अभीप्साओं का, आध्यात्मिक आकांक्षाओं का आंतरिक शत्रु बन जाता है। इसके विपरीत सोचें—हमारा अहंकेंद्रित व्यक्तित्व हमारे मन- मस्तिष्क के, हमारे हित के लिए निर्धारित निर्देशों और सहज प्रभुकृपावश मिले मार्गदर्शन का अनुकरण करने लगता है तो यह हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक, हमारी भरपूर सहायता करने वाला हमारा मित्र बन जाता है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण- ध्यान द्वारा अपने चित्त- मन का पर्यवेक्षण—परिशोधन अत्यंत अनिवार्य है। योगेश्वर इन दो श्लोकों (पाँचवें एवं छठे)द्वारा ध्यान की पृष्ठभूमि बना रहे हैं।
ध्यान की ही महिमा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा एक साधारण- सा, किंतु तार्किक नवयुवक जो बंगभूमि में जन्मा था, नरेंद्र जिसका नाम था, स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्धि पा सका। इसी ध्यान ने कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को, जो विषय- विलास भरे जीवन में जी रहे थे, आत्मबोध पाने को विवश किया। वे गौतम बुद्ध बनकर शांति और दया की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने आपे का बोध, अपने अंतर्जगत् में प्रवेश कर किया गया ध्यान मनुष्य के अव्यवस्थित व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित बना देता है, उसके जीवन को प्रज्वलित कर उसे बल- उत्साह और विधेयात्मक उल्लास से भर देता है—उसे अपने भाग्य का निर्माता बना देता है। ‘‘विश्वास नित्य प्रबल बनाओ कि तुम संसार के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, अपने भाग्य के विधाता हो।’’ यह वाक्य सदियों से ढेर सारे मनुष्यों को महामानव बनाने की प्रेरणा देता रहा है। इस वाक्य को परमपूज्य गुरुदेव ने सर्वाधिक महत्त्व दिया। स्वयं अपने जीवन में उनने ध्यान को स्थान देकर ‘मैं क्या हूँ’ (ह्वाट एम आई) पुस्तक लिखी, एक लंबी पुरश्चरण साधना (नित्य आठ हजार बार गायत्री जप, लगातार चौबीस वर्ष तक) संपन्न की एवं एक विराट् संगठन के निर्माण के निमित्त बने, जिसने इक्कीसवीं सदी- उज्ज्वल भविष्य का नारा दिया। सतत आशावादी चिंतन, अपने आपे को अधिकाधिक प्रबल- शक्तिपुंज बनाना, यह आचार्यश्री के जीवन में ही नहीं, उनकी प्रेरणाओं, लेखन व ओजस्वी वाणी में स्थान- स्थान पर दिखाई देता है।
आत्म निर्माण से युग निर्माण
युग निर्माण योजना का मूलमंत्र है—आत्मनिर्माण। हो सकता है कि दूसरे हमारा कहना नहीं मानें, पर हमारा अपना आपा तो हम जीत सकते हैं। ‘अपना सुधार ही संसार की सर्वश्रेष्ठ सेवा है’ वाक्य जन- जन को देने वाले परमपूज्य गुरुदेव ने बार- बार कहा कि हम यदि बदलेंगे, मजबूत बनेंगे, आत्मिक निर्माण की ओर चलेंगे, तो युग स्वतः बदलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न- विकसित देवमानवों का समुदाय खड़ा होने लगेगा। व्यक्ति- निर्माण से ही शुरुआत होती है, फिर परिवार- समाज इस क्रम से सारा विश्व नए विधान के अनुरूप खड़ा होने लगता है। परमपूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक ‘उद्धरेत्आत्मनाऽत्मानं’ में लिखते हैं, ‘‘अध्यात्म विद्या का प्रथम सूत्र यह है कि प्रत्येक भली- बुरी परिस्थिति का उत्तरदायी हम अपने आप को मानें। बाह्य समस्याओं का बीज अपने में ढूँढ़ें और जिस प्रकार का सुधार बाहरी घटनाओं- व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में चाहते हैं, उसी के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव में हेर- फेर प्रारंभ कर दें।’’ (पृष्ठ ३)
परमपूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, ‘‘कहावत है कि अपनी अक्ल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को सौगुनी दिखाई पड़ती है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष एवं पूर्ण बुद्धिमान मानता है। न तो उसे अपनी त्रुटियाँ सूझ पड़ती हैं और न अपनी समझ में कोई दोष दिखाई देता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुँचाई है, जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी नहीं पहुँचाई होगी।’’ (पृष्ठ ७)
पूज्यवर के इस चिंतन के साथ इस छठे श्लोक का मर्म यदि समझ लिया जाए, तो जीवन एक कलाकार की तरह जिया जा सकता है। जैसा हम सोचते हैं, विधेयात्मक या निषेधात्मक, हमारा आभामंडल वैसा ही बनता चला जाता है। जिसका मन जीता हुआ है, इंद्रियों पर, विषय- वासनाओं पर जिसका नियंत्रण है, वह निश्चित मानिए कि अपने आकर्षक आभामंडल से अगणित लोगों को प्रभावित कर उन्हें भी उसी दिशा में गतिशील कर देगा। जिसका मन इंद्रियों का गुलाम है, वह क्या तो किसी को प्रभावित करेगा, खुद ही उस प्रवाह में बहता रहेगा, अपने जीवनदेवता की दुर्गति करता दिखाई देगा। इस छठे अध्याय में ध्यान जैसे विषय पर आने से पूर्व आत्मसंयमयोग नामक इस अध्याय में योगेश्वर श्रीकृष्ण बार- बार व्यक्ति को अंतर्मुखी बन अपनी अंतर्जगत् की यात्रा करने हेतु सम्यक् मार्गदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य उनका एक ही है कि उसकी चित्तवृत्तियाँ गड़बड़ाने न पाएँ, वह वैचारिक प्रदूषण से भरे इस समाज में कम- से अपने चिंतन को ऊर्जावान बनाए रखे। दिव्यकर्मी के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है।
पराशांति को पाने का मार्ग
जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह किन्हीं भी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परिस्थितियाँ उसके लिए बाधित नहीं होतीं। उसका मनोबल इतना प्रचंड होता है कि वह फिर किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रह अपनी आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त करता चलता है। उसकी आत्मा उसके वश में होती है। यही नहीं, वह उस पराशांति को पहुँचा हुआ होता है, जहाँ उसकी परम आत्मा उसके सामने सहज ही प्रकट रहती है। श्री अरविंद के शब्दों में, ‘‘यह समाधिस्थ परम आत्मा सदा, हर पल, मन की जाग्रत् अवस्था में भी, जब वासना और अशांति के कारण मौजूद हों तब भी, शीत- उष्ण, सुख- दुःख तथा मान- अपमान आदि के प्रसंग होने पर भी अपनी वृत्तियों को भली- भाँति शांत बनाए रखता है।’’ श्री गीताजी अध्याय छः के सातवें श्लोक में इसी भाव को इस तरह स्पष्ट करती हैं —
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ६/७
पहले शब्दार्थ देखते हैं— जितेन्द्रिय(जितात्मनः) राग- द्वेषरहित मनुष्य का (प्रशान्तस्य) शुद्ध जीवात्मा (परमात्मा) शीत- उष्ण, सुख- दुःख आदि में (शीतोष्ण सुखदुःखेषु) तथा (तथा) मान और अपमान में (मानापमानयोः) सदैव आत्मसत्ता में ही निवेशित रहता है (समाहितः)।
अर्थात् वह व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भलीभाँति शांत हैं, उसका मन सरदी- गरमी, सुख- दुःख और मानापमान में निरंतर सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही नियोजित रहता है। (अध्याय ६, श्लोक ७)
परमात्मा समाहितः
इसका मतलब यह हुआ कि उसके ज्ञान में सिर्फ परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है एवं यह ध्यान से प्राप्त होती है, यह श्रीकृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। संयम की परिणति बड़ी विलक्षण है। इसका परिपालन करने पर हम सबके लिए वह दिव्य अनुभव संभव है, जिसमें हर क्षण हमें परमात्मा का सान्निध्य मिलता रहता है। ध्यान मात्र मन का व्यायाम या कसरत नहीं है, यह तो सीधे परमात्मा से संबंध स्थापित कराने वाली साधना है, पर यह इतनी आसान भी नहीं है। इसके लिए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं—(१) जिसने अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो (जितात्मनः), (२) जिसका मन पूर्णतः शांत हो (प्रशान्तस्य), वह सदैव परमात्मा की निरंतर बनी रहने वाली अनुभूति का लाभ लेता है (परमात्मा समाहितः)। फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उसका मन प्रचंड शक्ति से संपन्न होने के कारण जरा भी नहीं गड़बड़ाता। स्वयं पर नियंत्रण एवं मन की शांति—ऐसी दो अवस्थाएँ हैं, जिनसे हम इंद्रियों के बहिर्मुखी स्वभाव और मन- बुद्धि की बहिरंग प्रधान प्रवृत्तियों को नियमित बना पाते हैं। यह नियमन साधक के व्यक्तित्व के तीनों स्तर शरीर- मन, इन तीनों स्तरों पर होना है, इसीलिए गीताकार यहाँ मुहावरे का प्रयोग करते हैं ।। वे कहते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी या गरमी का वातावरण (शीत उष्णेषु) हो, सुख- दुःखप्रधान परिस्थितियाँ (सुखदुःखेषु)हों और मान- अपमान की (मानापमानयोः) स्थिति हो, वह सदैव परमात्मा में लीन रह अपने अंतरंग—मन को शांतिपूर्वक साधता हुआ जीवन जीता है। शीत- उष्ण की बात शरीर के स्तर पर, सुख- दुःख की बात मन के स्तर पर तथा मान- अपमान की बात बौद्धिक स्तर पर लागू होती है। ये अनुभव दोनों प्रकार के हो सकते हैं—अनुकूल भी, प्रतिकूल भी।
मुक्तपुरुष जो बिना किसी कामना या आसक्ति के कर्म करता है, उस पराशांति की स्थिति में पहुँचा हुआ होता है, जहाँ उसकी परमात्मसत्ता उसके सामने सतत विद्यमान रहती है। यह सत्ता मन की जाग्रत् अवस्था में भी, वासना और अशांति की परिस्थितियों के मौजूद होते हुए भी तथा शीतोष्ण, सुख- दुःख, मानापमान आदि द्वंद्वों की स्थिति में भी समाहित रहती है। यह मनुष्य की उच्चतर विकसित स्थिति है।
ध्यानयोग की पूर्व तैयारी
वस्तुतः दिव्यकर्मी साधक, जिसे श्रीकृष्ण ध्यान करना सिखा रहे हैं, इस समय अर्जुन के रूप में उनके समक्ष मौजूद है। हम सबका वह एक प्रतीकरूप में माध्यम है, अपने गुरु योगेश्वर से यह जानना चाह रहा है कि जब मैं इस स्थिति में प्रवेश करूँगा तो क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? श्रीकृष्ण तो मन को पढ़ लेते हैं। अभी अर्जुन का एक प्रश्र थोड़ी देर बाद प्रतीक्षित है, जिसमें वह मन की चंचलता की बात कहता है; किंतु उससे भी पूर्व श्रीकृष्ण उसे ध्यानयोग की तैयारी के विषय में बता रहे हैं। जब व्यक्ति चित्त में प्रवेश करता है तो चित्त के संस्कार, कई प्रकार की यादें, अतृप्त कामनाएँ मस्तिष्क- पटल पर आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में दिखने वाला मन व देखने वाला मन दोनों ही द्रष्टा बन जाते हैं। यदि इंद्रियाँ मजबूत नहीं हुईं, उन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ध्यान लगाना तो दूर, कई प्रकार के चित्र- विचित्र दृश्य कुसंस्कारों के ‘प्रोजेक्शन’ के रूप में दिखाई देने लगेंगे। हमारा अचेतन परिष्कृत हो, इंद्रियाँ हमारी अपने ही नियंत्रण में हों तथा हम शांत मनःस्थिति में हों, तो हमारे ध्यानस्थ होने की तैयारी पूरी हो जाती है। जब मनुष्य संसार की आसक्तियों से हटकर भगवान् की ओर बढ़ता है, तो उसका मन धीरे- धीरे शांत होने लगता है। श्री रामकृष्ण परहंस के अनुसार, ‘‘जैसे- जैसे हम काशी की ओर बढ़ते हैं, कलकत्ता पीछे छूटता चला जाता है।’’ इस पंक्ति के पीछे संकेत है कि जैसे- जैसे भोगवाद से पीछा छूटता है, व्यक्ति मन की शांति, आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ने लगता है।
शान्त मनःस्थिति एक उपलब्धि
सांसारिकता में रमा मन हानि- लाभ, सुख- दुःख, मान- अपमान से तो प्रभावित होता है; परंतु जैसे- जैसे आध्यात्मिकता का रंग चढ़ने लगता है, मनुष्य क्रमशः इनसे परे हो जाता है। जैसे ही इन भौतिक कारणों से स्वयं को परे किया, व्यक्ति का मन उसी अनुपात में शांत होता चला जाता है। सातवें श्लोक का मर्म यह है कि तुम स्वयं को परमात्मा को अर्पित कर दो, फिर लौकिक दुःख तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारी मनःस्थिति को तनावग्रस्त नहीं होने देंगे। कर्मयोग के साथ शरणागति का भाव बार- बार अपनाने हेतु प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं और उस दिव्य अनुभव का लाभ लेने हेतु संकेत कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या उनने अगले आठवें श्लोक में की है। इसकी चर्चा बाद में, अभी अपने मन को जीतने की चर्चा पूरी करें। भगवान ने छठे श्लोक में कहा कि जिसका मन और चित्त पूरी तरह जीत लिया गया है, उसका वह मित्र है। कोई भी जानना चाहेगा, यह मित्र बनाने का उपाय। यह उपाय वे सातवें श्लोक में बताते हैं कि संसार से मन को हटाते चलो, परमात्मा में उसे अर्पण करते चलो। फिर कुछ भी तुम्हें व्यापेगा नहीं—न मान, न अपमान, न दुःख, न सुख। बुद्ध व महावीर की चित्तवृत्तियाँ भगवान् में विलीन हो गई थीं। साधारण सांसारिक मनुष्यों ने उन्हें गाली दी, अपशब्द कहे, पर वे सतत् प्रसन्न। वे जानते थे कि उनके दुर्वचन उन्हें क्यों व्यापेंगे, वे तो परमात्मसत्ता में लीन, सदैव प्रसन्न एवं शांत मनःस्थिति के प्राणी थे। सचमुच वे परमात्मारूप ही हो गए थे। गीता में आत्मसंयमयोग की यात्रा आत्मा की परमात्मा से तद्रूप होने की यात्रा है।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ ६/६
इसका शब्दार्थ देखें—
जिस (येन) विवेकयुक्त बुद्धि द्वारा (आत्मना) मन ही (आत्मा एव) जीत लिया है—वशीभूत कर लिया गया है (जितः), मन (आत्मा)उसके (तस्य) जीवात्मा का (आत्मनः) मित्र है (बन्धुः, किंतु (तु) अवशीभूत व्यक्ति का (अनात्मनः) मन (आत्मा) शत्रु की तरह (शत्रुवत्) शत्रुता का आचरण करने में (शत्रुत्वे) प्रवृत्त हो जाता है (वर्तते)।
अर्थात् जिसने अपने आत्मा द्वारा अपने मन एवं इन्द्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, उसके लिए यह आत्मा मित्र है; किंतु जिसने अपने आत्मा को जीता नहीं है, उसका आत्मा ही उसका विरोधी हो जाता है और उसके प्रति बाह्य शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जीव को वह हर प्रकार की हानि पहुँचाता है। (श्लोक ६, अध्याय ६)
कितनी सुंदर उत्तरार्द्धपरक चर्चा इस श्लोक में आई है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसके लिए उसका बौद्धिक व्यक्तित्व मित्र है (बन्धुरात्मात्मनस्तस्य) और यदि हम किसी कारणवश अपने मन, इन्द्रियों, बुद्धि वाले पक्ष पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो, यह अविजित बुद्धि ही हमारे विरुद्ध एक भयावह अजेय शत्रु की तरह काम करती है। यहाँ वह अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य का अपना आपा कब मित्र हो जाता है, कब शत्रु। जिसने अपने को जीत लिया, अपनी इंद्रियों पर अपना स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसका मन उसका मित्र है। संसार की आसक्तियों से स्वयं को हटाते चलना एवं भगवान् में मन लगाते चलना, सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्वयं को सम्यक् रूप में स्थित करना ही एकमात्र बंधनमुक्ति का उपाय है।
मित्र- शत्रु हमारे अपने ही अंदर
हम स्वभाव से बहिर्मुखी हैं। अपने मित्र एवं शत्रु हम बाहर ही ढूँढ़ते रहते हैं। वस्तुतः बाहर—बहिरंग जगत् में न तो हमारा कोई मित्र है और न कोई शत्रु ही है। ये सभी हमारे भीतर अंतरंग में विद्यमान हैं। हमारा अपना अहं जो अनुशासनों के पालन की बात आने पर बाधक बनने लगता है तथा हमारे अपने बौद्धिक व्यक्तित्व- परिष्कृत आत्मतत्त्व के मार्गदर्शन में चलने से इनकार कर देता है तो यह हमारी अभीप्साओं का, आध्यात्मिक आकांक्षाओं का आंतरिक शत्रु बन जाता है। इसके विपरीत सोचें—हमारा अहंकेंद्रित व्यक्तित्व हमारे मन- मस्तिष्क के, हमारे हित के लिए निर्धारित निर्देशों और सहज प्रभुकृपावश मिले मार्गदर्शन का अनुकरण करने लगता है तो यह हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक, हमारी भरपूर सहायता करने वाला हमारा मित्र बन जाता है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण- ध्यान द्वारा अपने चित्त- मन का पर्यवेक्षण—परिशोधन अत्यंत अनिवार्य है। योगेश्वर इन दो श्लोकों (पाँचवें एवं छठे)द्वारा ध्यान की पृष्ठभूमि बना रहे हैं।
ध्यान की ही महिमा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा एक साधारण- सा, किंतु तार्किक नवयुवक जो बंगभूमि में जन्मा था, नरेंद्र जिसका नाम था, स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्धि पा सका। इसी ध्यान ने कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को, जो विषय- विलास भरे जीवन में जी रहे थे, आत्मबोध पाने को विवश किया। वे गौतम बुद्ध बनकर शांति और दया की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने आपे का बोध, अपने अंतर्जगत् में प्रवेश कर किया गया ध्यान मनुष्य के अव्यवस्थित व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित बना देता है, उसके जीवन को प्रज्वलित कर उसे बल- उत्साह और विधेयात्मक उल्लास से भर देता है—उसे अपने भाग्य का निर्माता बना देता है। ‘‘विश्वास नित्य प्रबल बनाओ कि तुम संसार के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, अपने भाग्य के विधाता हो।’’ यह वाक्य सदियों से ढेर सारे मनुष्यों को महामानव बनाने की प्रेरणा देता रहा है। इस वाक्य को परमपूज्य गुरुदेव ने सर्वाधिक महत्त्व दिया। स्वयं अपने जीवन में उनने ध्यान को स्थान देकर ‘मैं क्या हूँ’ (ह्वाट एम आई) पुस्तक लिखी, एक लंबी पुरश्चरण साधना (नित्य आठ हजार बार गायत्री जप, लगातार चौबीस वर्ष तक) संपन्न की एवं एक विराट् संगठन के निर्माण के निमित्त बने, जिसने इक्कीसवीं सदी- उज्ज्वल भविष्य का नारा दिया। सतत आशावादी चिंतन, अपने आपे को अधिकाधिक प्रबल- शक्तिपुंज बनाना, यह आचार्यश्री के जीवन में ही नहीं, उनकी प्रेरणाओं, लेखन व ओजस्वी वाणी में स्थान- स्थान पर दिखाई देता है।
आत्म निर्माण से युग निर्माण
युग निर्माण योजना का मूलमंत्र है—आत्मनिर्माण। हो सकता है कि दूसरे हमारा कहना नहीं मानें, पर हमारा अपना आपा तो हम जीत सकते हैं। ‘अपना सुधार ही संसार की सर्वश्रेष्ठ सेवा है’ वाक्य जन- जन को देने वाले परमपूज्य गुरुदेव ने बार- बार कहा कि हम यदि बदलेंगे, मजबूत बनेंगे, आत्मिक निर्माण की ओर चलेंगे, तो युग स्वतः बदलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न- विकसित देवमानवों का समुदाय खड़ा होने लगेगा। व्यक्ति- निर्माण से ही शुरुआत होती है, फिर परिवार- समाज इस क्रम से सारा विश्व नए विधान के अनुरूप खड़ा होने लगता है। परमपूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक ‘उद्धरेत्आत्मनाऽत्मानं’ में लिखते हैं, ‘‘अध्यात्म विद्या का प्रथम सूत्र यह है कि प्रत्येक भली- बुरी परिस्थिति का उत्तरदायी हम अपने आप को मानें। बाह्य समस्याओं का बीज अपने में ढूँढ़ें और जिस प्रकार का सुधार बाहरी घटनाओं- व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में चाहते हैं, उसी के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव में हेर- फेर प्रारंभ कर दें।’’ (पृष्ठ ३)
परमपूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, ‘‘कहावत है कि अपनी अक्ल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को सौगुनी दिखाई पड़ती है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष एवं पूर्ण बुद्धिमान मानता है। न तो उसे अपनी त्रुटियाँ सूझ पड़ती हैं और न अपनी समझ में कोई दोष दिखाई देता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुँचाई है, जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी नहीं पहुँचाई होगी।’’ (पृष्ठ ७)
पूज्यवर के इस चिंतन के साथ इस छठे श्लोक का मर्म यदि समझ लिया जाए, तो जीवन एक कलाकार की तरह जिया जा सकता है। जैसा हम सोचते हैं, विधेयात्मक या निषेधात्मक, हमारा आभामंडल वैसा ही बनता चला जाता है। जिसका मन जीता हुआ है, इंद्रियों पर, विषय- वासनाओं पर जिसका नियंत्रण है, वह निश्चित मानिए कि अपने आकर्षक आभामंडल से अगणित लोगों को प्रभावित कर उन्हें भी उसी दिशा में गतिशील कर देगा। जिसका मन इंद्रियों का गुलाम है, वह क्या तो किसी को प्रभावित करेगा, खुद ही उस प्रवाह में बहता रहेगा, अपने जीवनदेवता की दुर्गति करता दिखाई देगा। इस छठे अध्याय में ध्यान जैसे विषय पर आने से पूर्व आत्मसंयमयोग नामक इस अध्याय में योगेश्वर श्रीकृष्ण बार- बार व्यक्ति को अंतर्मुखी बन अपनी अंतर्जगत् की यात्रा करने हेतु सम्यक् मार्गदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य उनका एक ही है कि उसकी चित्तवृत्तियाँ गड़बड़ाने न पाएँ, वह वैचारिक प्रदूषण से भरे इस समाज में कम- से अपने चिंतन को ऊर्जावान बनाए रखे। दिव्यकर्मी के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है।
पराशांति को पाने का मार्ग
जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह किन्हीं भी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परिस्थितियाँ उसके लिए बाधित नहीं होतीं। उसका मनोबल इतना प्रचंड होता है कि वह फिर किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रह अपनी आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त करता चलता है। उसकी आत्मा उसके वश में होती है। यही नहीं, वह उस पराशांति को पहुँचा हुआ होता है, जहाँ उसकी परम आत्मा उसके सामने सहज ही प्रकट रहती है। श्री अरविंद के शब्दों में, ‘‘यह समाधिस्थ परम आत्मा सदा, हर पल, मन की जाग्रत् अवस्था में भी, जब वासना और अशांति के कारण मौजूद हों तब भी, शीत- उष्ण, सुख- दुःख तथा मान- अपमान आदि के प्रसंग होने पर भी अपनी वृत्तियों को भली- भाँति शांत बनाए रखता है।’’ श्री गीताजी अध्याय छः के सातवें श्लोक में इसी भाव को इस तरह स्पष्ट करती हैं —
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ६/७
पहले शब्दार्थ देखते हैं— जितेन्द्रिय(जितात्मनः) राग- द्वेषरहित मनुष्य का (प्रशान्तस्य) शुद्ध जीवात्मा (परमात्मा) शीत- उष्ण, सुख- दुःख आदि में (शीतोष्ण सुखदुःखेषु) तथा (तथा) मान और अपमान में (मानापमानयोः) सदैव आत्मसत्ता में ही निवेशित रहता है (समाहितः)।
अर्थात् वह व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भलीभाँति शांत हैं, उसका मन सरदी- गरमी, सुख- दुःख और मानापमान में निरंतर सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही नियोजित रहता है। (अध्याय ६, श्लोक ७)
परमात्मा समाहितः
इसका मतलब यह हुआ कि उसके ज्ञान में सिर्फ परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है एवं यह ध्यान से प्राप्त होती है, यह श्रीकृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। संयम की परिणति बड़ी विलक्षण है। इसका परिपालन करने पर हम सबके लिए वह दिव्य अनुभव संभव है, जिसमें हर क्षण हमें परमात्मा का सान्निध्य मिलता रहता है। ध्यान मात्र मन का व्यायाम या कसरत नहीं है, यह तो सीधे परमात्मा से संबंध स्थापित कराने वाली साधना है, पर यह इतनी आसान भी नहीं है। इसके लिए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं—(१) जिसने अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो (जितात्मनः), (२) जिसका मन पूर्णतः शांत हो (प्रशान्तस्य), वह सदैव परमात्मा की निरंतर बनी रहने वाली अनुभूति का लाभ लेता है (परमात्मा समाहितः)। फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उसका मन प्रचंड शक्ति से संपन्न होने के कारण जरा भी नहीं गड़बड़ाता। स्वयं पर नियंत्रण एवं मन की शांति—ऐसी दो अवस्थाएँ हैं, जिनसे हम इंद्रियों के बहिर्मुखी स्वभाव और मन- बुद्धि की बहिरंग प्रधान प्रवृत्तियों को नियमित बना पाते हैं। यह नियमन साधक के व्यक्तित्व के तीनों स्तर शरीर- मन, इन तीनों स्तरों पर होना है, इसीलिए गीताकार यहाँ मुहावरे का प्रयोग करते हैं ।। वे कहते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी या गरमी का वातावरण (शीत उष्णेषु) हो, सुख- दुःखप्रधान परिस्थितियाँ (सुखदुःखेषु)हों और मान- अपमान की (मानापमानयोः) स्थिति हो, वह सदैव परमात्मा में लीन रह अपने अंतरंग—मन को शांतिपूर्वक साधता हुआ जीवन जीता है। शीत- उष्ण की बात शरीर के स्तर पर, सुख- दुःख की बात मन के स्तर पर तथा मान- अपमान की बात बौद्धिक स्तर पर लागू होती है। ये अनुभव दोनों प्रकार के हो सकते हैं—अनुकूल भी, प्रतिकूल भी।
मुक्तपुरुष जो बिना किसी कामना या आसक्ति के कर्म करता है, उस पराशांति की स्थिति में पहुँचा हुआ होता है, जहाँ उसकी परमात्मसत्ता उसके सामने सतत विद्यमान रहती है। यह सत्ता मन की जाग्रत् अवस्था में भी, वासना और अशांति की परिस्थितियों के मौजूद होते हुए भी तथा शीतोष्ण, सुख- दुःख, मानापमान आदि द्वंद्वों की स्थिति में भी समाहित रहती है। यह मनुष्य की उच्चतर विकसित स्थिति है।
ध्यानयोग की पूर्व तैयारी
वस्तुतः दिव्यकर्मी साधक, जिसे श्रीकृष्ण ध्यान करना सिखा रहे हैं, इस समय अर्जुन के रूप में उनके समक्ष मौजूद है। हम सबका वह एक प्रतीकरूप में माध्यम है, अपने गुरु योगेश्वर से यह जानना चाह रहा है कि जब मैं इस स्थिति में प्रवेश करूँगा तो क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? श्रीकृष्ण तो मन को पढ़ लेते हैं। अभी अर्जुन का एक प्रश्र थोड़ी देर बाद प्रतीक्षित है, जिसमें वह मन की चंचलता की बात कहता है; किंतु उससे भी पूर्व श्रीकृष्ण उसे ध्यानयोग की तैयारी के विषय में बता रहे हैं। जब व्यक्ति चित्त में प्रवेश करता है तो चित्त के संस्कार, कई प्रकार की यादें, अतृप्त कामनाएँ मस्तिष्क- पटल पर आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में दिखने वाला मन व देखने वाला मन दोनों ही द्रष्टा बन जाते हैं। यदि इंद्रियाँ मजबूत नहीं हुईं, उन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ध्यान लगाना तो दूर, कई प्रकार के चित्र- विचित्र दृश्य कुसंस्कारों के ‘प्रोजेक्शन’ के रूप में दिखाई देने लगेंगे। हमारा अचेतन परिष्कृत हो, इंद्रियाँ हमारी अपने ही नियंत्रण में हों तथा हम शांत मनःस्थिति में हों, तो हमारे ध्यानस्थ होने की तैयारी पूरी हो जाती है। जब मनुष्य संसार की आसक्तियों से हटकर भगवान् की ओर बढ़ता है, तो उसका मन धीरे- धीरे शांत होने लगता है। श्री रामकृष्ण परहंस के अनुसार, ‘‘जैसे- जैसे हम काशी की ओर बढ़ते हैं, कलकत्ता पीछे छूटता चला जाता है।’’ इस पंक्ति के पीछे संकेत है कि जैसे- जैसे भोगवाद से पीछा छूटता है, व्यक्ति मन की शांति, आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ने लगता है।
शान्त मनःस्थिति एक उपलब्धि
सांसारिकता में रमा मन हानि- लाभ, सुख- दुःख, मान- अपमान से तो प्रभावित होता है; परंतु जैसे- जैसे आध्यात्मिकता का रंग चढ़ने लगता है, मनुष्य क्रमशः इनसे परे हो जाता है। जैसे ही इन भौतिक कारणों से स्वयं को परे किया, व्यक्ति का मन उसी अनुपात में शांत होता चला जाता है। सातवें श्लोक का मर्म यह है कि तुम स्वयं को परमात्मा को अर्पित कर दो, फिर लौकिक दुःख तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारी मनःस्थिति को तनावग्रस्त नहीं होने देंगे। कर्मयोग के साथ शरणागति का भाव बार- बार अपनाने हेतु प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं और उस दिव्य अनुभव का लाभ लेने हेतु संकेत कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या उनने अगले आठवें श्लोक में की है। इसकी चर्चा बाद में, अभी अपने मन को जीतने की चर्चा पूरी करें। भगवान ने छठे श्लोक में कहा कि जिसका मन और चित्त पूरी तरह जीत लिया गया है, उसका वह मित्र है। कोई भी जानना चाहेगा, यह मित्र बनाने का उपाय। यह उपाय वे सातवें श्लोक में बताते हैं कि संसार से मन को हटाते चलो, परमात्मा में उसे अर्पण करते चलो। फिर कुछ भी तुम्हें व्यापेगा नहीं—न मान, न अपमान, न दुःख, न सुख। बुद्ध व महावीर की चित्तवृत्तियाँ भगवान् में विलीन हो गई थीं। साधारण सांसारिक मनुष्यों ने उन्हें गाली दी, अपशब्द कहे, पर वे सतत् प्रसन्न। वे जानते थे कि उनके दुर्वचन उन्हें क्यों व्यापेंगे, वे तो परमात्मसत्ता में लीन, सदैव प्रसन्न एवं शांत मनःस्थिति के प्राणी थे। सचमुच वे परमात्मारूप ही हो गए थे। गीता में आत्मसंयमयोग की यात्रा आत्मा की परमात्मा से तद्रूप होने की यात्रा है।
Versions
-
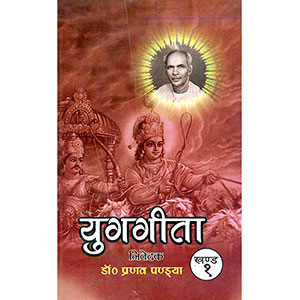
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
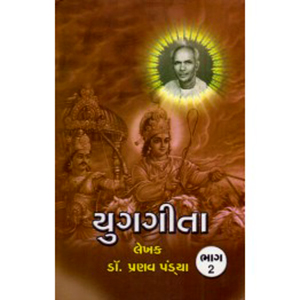
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
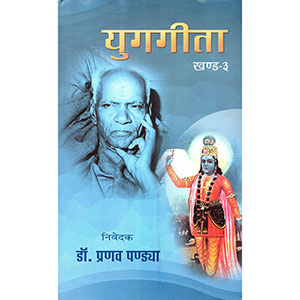
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
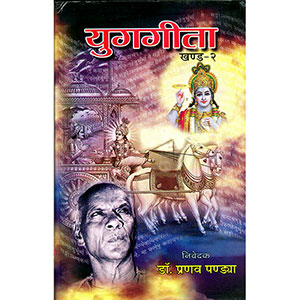
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
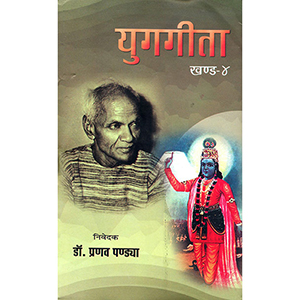
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
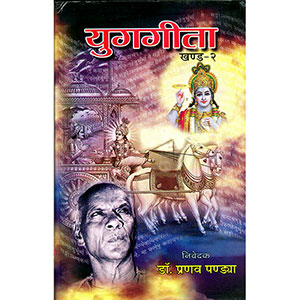
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
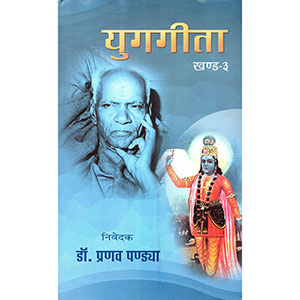
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
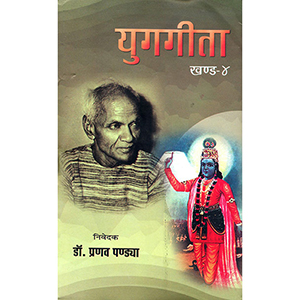
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
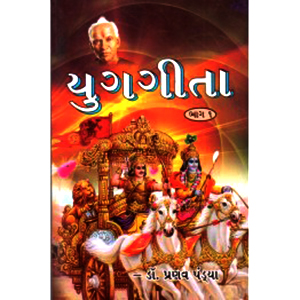
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रस्तुत तृतीय खण्ड की प्रस्तावना
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- कर्मसंन्यास एवं कर्मयोग में कौन सा श्रेष्ठ है?
- सांख्य (संन्यास) और कर्मयोग दोनों एक ही हैं, अलग-अलग नहीं
- कर्मयोग के अभ्यास बिना संन्यास सधेगा नहीं
- कर्त्ताभाव से मुक्त द्रष्टा स्तर का दिव्यकर्मी
- कर्मयोग की परमसिद्धि-अंतःशुद्धि
- न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते
- निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
- आदर्शनिष्ठ महामानव कैसे बनें
- ब्रह्म में प्रतिष्ठित संवेदनशील दिव्यकर्मी
- ज्ञानीजन क्षणिक सुखों में रमण नहीं करते
- योगेश्वर का प्रकाश-स्तंभ बनने हेतु भावभरा आमंत्रण
- परम शांतिरूपी मुक्ति का एकमात्र मार्ग
- ‘महावाक्य’ से समापन होता है, कर्म संन्यास योग की व्याख्या का
- संकल्पों से मुक्ति मिले, तो योग सधे
- योगारूढ़ होकर ही मन को शांत किया जा सकता है
- उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्
- जीता हुआ मन ही हमारा सच्चा मित्र
- कैसे बनें पूरी तरह युक्तपुरुष

