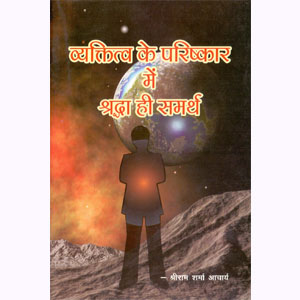व्यक्तित्व परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ 
श्रद्धा-संवर्धन में समर्थ ब्रह्मविद्या
Read Scan Version
सांसारिक सुखों की उपलब्धि के लिए शरीर-बल आवश्यक है। धन हो तो प्रत्येक मनोवांछित वस्तु सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। जन-शक्ति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति तक सत्तारूढ़ हुए हैं। चातुर्य, पद, सत्ता आदि से कोई भी व्यक्ति मनचाही इच्छायें पूरी कर सकता है, किन्तु ज्ञान के अभाव में यह सारी शक्तियां लघु प्रतीत होती हैं। ज्ञान संसार का सर्वोत्तम बल है। इसी के आधार पर दूसरी सफलतायें प्राप्त की जा सकती हैं। अज्ञान-वश मनुष्य तन-धन-जन सभी का नाश कर लेता है। दुष्कर्म में लगे व्यक्ति का कहां तो शरीर ठीक रहेगा, कितने दिन धन ठहरेगा और कब तक दूसरों का सहयोग-सहानुभूति व आत्मीयता मिलेगी? मनुष्य ज्ञान के अभाव में ही बुरे कर्मों की ओर प्रेरित होता है। इसलिए संसार में ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बल कहा गया है।
बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम साधनों में भी सुखी दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि अज्ञानता के दुष्परिणामों से बचे रहते हैं। उनके प्रत्येक कार्य में विवेक होता है, जो कुछ करते हैं उसे पहले भली प्रकार सोच समझ लेते हैं। पूरी तरह विचार करने के बाद किये गये कार्यों में हानि की सम्भावना प्रायः समाप्त हो जाती है और उस कार्य में पड़ने वाली बाधाओं, परेशानियों और मुसीबतों से बचने का रास्ता मिल जाता है। ज्ञान मनुष्य को जीवन का सही रास्ता प्रदर्शित करता है जिससे उसे कठिनाइयां कम होती और सफलतायें अधिक मिलती हैं। कदाचित् परिस्थितिवश कोई विघ्न आ भी जाए तो अपनी दूरदर्शिता के कारण बुद्धिमान व्यक्ति उसे आसानी से हल कर लेते हैं। ओछे कर्म करने वाले लोगों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि ऐसे कार्य वे अधिकांश अज्ञानतावश ही करते हैं। जीवन की सही दिशा निर्माण करने की क्षमता न तो धन में है, न पद में न प्रतिष्ठा में। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया सत्कर्मों से पूरी होती है। सन्मार्ग में भी कोई स्वतः प्रवृत्त होता हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। यह प्रेरणा हमें औरों से मिलती है। दूसरों की अच्छाइयों का अनुकरण करते हुए ही महानता की मंजिल तक पहुंचने का नियम बना हुआ है। ऐसी बुद्धि किसी को मिल जाए तो उसे यही समझना चाहिए कि परमात्मा की उस पर बड़ी कृपा है। ज्ञान से मनुष्य की ऐसी ही धर्म बुद्धि जागृत होती है। इसलिए ज्ञान को परमात्मा का सर्वोत्तम वरदान मानना पड़ता है।
अज्ञानता के दुष्परिणाम से बचने का यह तरीका सबसे अच्छा है कि हम अपनी मानसिक चेष्टाओं को संसार का रहस्य समझने में लगायें। विचार करने की शक्ति हमें इसीलिए मिली है कि हम सृष्टि की वस्तु स्थिति को समझें और इसका लाभ अपने सजातियों को भी दें, किन्तु यह सब कुछ तभी संभव है जब हमारा ज्ञान बढ़े। जब-तक हम ज्ञानवान् नहीं बनते, अज्ञानता का शैतान हमारे पीछे पड़ा रहेगा, ऐसी अवस्था में हमारी मोह-ग्रन्थियां ज्यों की त्यों बंधी रहेंगी। अज्ञानता का अंधकार और विश्व-रहस्य की जानकारी के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसी से भव-बन्धन टूटते हैं।
व्यक्ति के पात्रत्व की सच्ची कसौटी उसके ज्ञान से होती है। समाज में अधिक देर तक सम्मान व प्रतिष्ठा उन्हीं को मिलती है जो शीलवान, शिष्ट व विनम्र होते हैं। उद्दण्ड दुराचारी व अशिष्ट व्यक्तियों को सभी जगह तिरस्कार ही मिलता है। इन आध्यात्मिक सद्गुणों का आन्तिरिक प्रतिष्ठान ज्ञान से होता है इससे सदाचार में रुचि बढ़ती है। आप्त वचन है ‘‘विद्या ददाति विनयमं, विनयमं ददाति पात्रताम्’’ अर्थात् विद्या से ज्ञान से विनयशीलता आती है। विनयशील ही पात्रत्व के सच्चे अधिकारी होते हैं। मानवीय प्रतिभा का विकास ज्ञान से होता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के महान् व्यक्तित्व का विकास ज्ञान से हुआ है। भगवान् राम, कृष्ण, गौतमबुद्ध, ईसामसीह, सुकरात आदि सभी महापुरुषों ने ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। सांसारिक दुःखों से परित्राण पाने के लिए मानव जाति को सदैव ही इसकी आवश्यकता हुई है। शास्त्रकार ने ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है—
मोक्षस्य न हि वासेस्ति न ग्रामान्तर मेव वा। अज्ञान हृदयग्रन्थिर्नाशो मोक्ष इति स्मृत॥ (शिव-गीता)
अर्थात् मोक्ष किसी स्थान विशेष में उपलब्ध नहीं होता। इसे पाने के लिए गांव-गांव भटकने की भी आवश्यकता नहीं। हृदय की अज्ञान ग्रन्थि का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग, मुक्ति का साधन है—ज्ञान। इसे पा लिया तो इसी जीवन में जीवन-मुक्ति मिल गयी समझनी चाहिए।
इस युग में विज्ञान की शाखा प्रशाखायें सर्वत्र फैली हैं। प्रकाश, ताप, स्वर, विद्युत चुम्बकत्व और पदार्थों की जितनी वैज्ञानिक शोध इस युग में हुई है उसी को ज्ञान मानने की आज परम्परा चल पड़ी है। इसी के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन भी हो रहा है। तथाकथित विज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल सभी कर रहे हैं किन्तु यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि ज्ञान, बुद्धि की उस सूक्ष्म क्रियाशीलता का नाम है जो मनुष्य को सन्मार्ग की दिशा में प्रेरित करती है। विज्ञान का फल है इहलौकिक कामना पूर्ति और ज्ञान का सम्बन्ध है अन्तर्जगत से। ज्ञान वह है जो मनुष्य को आत्म-दर्शन में लगाये।
इसके लिए प्रमाद को त्याग कर विनम्र बनना पड़ता है। जो केवल अपनी अहंता प्रतिपादित करते रहते हैं, जिन्हें केवल अहंकार प्यारा है वे अपने संकुचित दृष्टिकोण के कारण ज्ञान के आनन्द और अनुभूति को जान नहीं पाते। छोटे से छोटा बन जाने पर ही महानता की पहचान की जा सकती है। गल्ले के भारी ढेर पंसेरियों में तौले जाते हैं। कपड़ों के थान गजों से नापते हैं। अमुक स्थान कितनी दूर है, यह मील के पत्थर बताते हैं। ऐसे ही विराट के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए महानता के गठबन्धन करने के लिए— हमें विनम्र बनना पड़ता है। भय, लज्जा और संकोच को त्यागकर तत्परतापूर्वक अपनी चेष्टाओं को उस ओर मोड़ना पड़ता है। तब कहीं ज्ञानवान् बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
अपने पास धन हो तो संसार की अनेकों वस्तुएं क्रय की जा सकती हैं। शारीरिक शक्ति हो तो दूसरों पर रौब जमाया जा सकता है। इससे दूसरों पर शासन भी कर सकते हैं औरों के अधिकारों का अपहरण भी कोई बलशाली कर सकता है। किन्तु विद्या किसी से खरीदी नहीं जा सकती दूसरों से छीन भी नहीं सकते। इसके लिए एकान्त में रहकर निरन्तर शोध, अध्ययन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अपनी मानसिक चेष्टाओं को सरस व मनोरंजक कार्यक्रमों से मोड़कर इसमें लगाना पड़ता है। ज्ञानार्जन एक महान् तप है। इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ता, मनस्विता और अध्ययन शीलता अपेक्षित हैं। इसे प्राप्त करने के बाद खो जाने का भय नहीं रहता। किन्हीं बालकों में किशोरावस्था में ही अलौकिक क्षमता या प्रतिभा देखते हैं तो यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि एक ही वय, स्थान व वातावरण में अनुकूल स्थिति प्राप्त होने पर भी दो बालकों की मानसिक शक्ति में यह अन्तर क्यों होता है? तब यह मानना पड़ता है कि एक में पूर्व जन्मों के ज्ञान के संस्कार प्रबल होते हैं दूसरे में क्षीण। भरत, ध्रुव, प्रह्लाद, अभिमन्यु आदि में जन्म से ही प्रखर ज्ञान के उज्ज्वल संस्कार पड़े थे। जगद्गुरु शंकराचार्य ने थोड़ी ही अवस्था में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। यह उनके पिछले जन्मों के परिपक्व ज्ञान के कारण ही हुआ मानना पड़ता है। इससे इस मत की पुष्टि होती है कि चिर-सहयोगी के रूप में जन्म-जन्मान्तरों तक साथ रहने वाला अपना ज्ञान ही है। ज्ञान का नाश नहीं होता। वह अजर है अमर है।
सार्थक जीवन की आधार-शिला ज्ञान है। बुद्धिमत्ता की सच्ची कसौटी यह है कि मनुष्य अपनी सच्ची जीवन दिशा निर्धारित करे। कुछ न कुछ करते रहें चाहें वह अहितकर ही क्यों न हो, यह बात तर्क-संगत प्रतीत नहीं होती। कर्म का महत्व तब है जब उससे हमें अपना जीवन-लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन में सन्मार्ग पर चलने से पूरी होती है। और सन्मार्ग पर देर तक टिके रहना ज्ञान-प्राप्ति से ही सम्भव है। ज्ञान ही इस संसार की सर्वोपरि सम्पत्ति है।
आत्मिक प्रगति के लिए-उत्कृष्ट शिक्षा की आवश्यकता
हमारे जीवन-यापन की क्रियाओं में पाप का पुट प्रवेश न करने पावे- इस सावधानी के लिये ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है। ज्ञान से दृष्टिकोण परिमार्जित होता है, विचार-शक्ति बढ़ती है और युक्तायुक्त निर्णय की क्षमता प्राप्त होती है। क्या पाप है, क्या पाप नहीं है, इसका ज्ञान जीवन एवं कर्म-दर्शन सम्बन्धी पुस्तकों से ही प्राप्त हो सकता है—और वे सद् ग्रन्थ हैं वेद-शास्त्र, गीता, उपनिषद्, रामायण आदि आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुस्तकें इन आर्ष ग्रन्थों के अतिरिक्त लौकिक विद्वानों द्वारा लिखा हुआ एक से एक बढ़कर नैतिक साहित्य भरा पड़ा है—योग्यता तथा युग के अनुसार उसका लाभ भी उठाया जा सकता है।
ज्ञान-गुण प्राप्त करने के लिये जिस वस्तु की प्रथम एवं प्रमुख आवश्यकता है, वह है—शिक्षा। शिक्षा ज्ञान की आधार भूमि है। जो अशिक्षित है, पढ़ा-लिखा नहीं है, वह किसी भी जीवन अथवा कर्म-दर्शन सम्बन्धी पुस्तक का अध्ययन किस प्रकार कर सकता है, किस प्रकार उनकी शिक्षाओं को समझ सकता है और किस प्रकार हृदयंगम कर सकता है? उसके लिये तो ज्ञान से भरी पुस्तकें भी रद्दी कागज से अधिक कोई मूल्य न रखेंगी।
अनेक लोग कबीर दादू, नानक, तुकाराम, रैदास, नरसी यहां तक कि सुकरात, मुहम्मद और ईसा जैसे महात्माओं एवं महापुरुषों का उदाहरण देकर कह सकते हैं कि यह लोग शिक्षित न होने पर भी पूर्ण ज्ञानवान् तथा आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। इनका सम्पूर्ण जीवन आजीवन निष्पाप रहा और निश्चय ही उन्होंने आत्मा को बन्धन मुक्त कर मोक्ष पद पाया है। इससे सिद्ध होता है कि निष्पाप जीवन की सिद्धि के लिये शिक्षा अनिवार्य नहीं है। ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि अनायास ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष अपने पूर्वजन्म के संस्कार साथ लेकर आते हैं।
एक ही शरीर में जीवन की इतिश्री नहीं हो जाती। इसका क्रम जन्म-जन्मान्तरों तक चला करता है और तब तक चलता रहता है, जब तक जीवात्मा पूर्ण निष्पाप होकर मुक्त नहीं हो जाती। अनायास ज्ञानज्ञों का उदाहरण देने वालों को विश्वास रखना चाहिए कि उक्त महात्माओं ने अपने पूर्वजन्मों में ज्ञान पाने के लिये अनर्थक पुरुषार्थ किया होता है। उसके इतने अनुपम एवं उर्वर बीज बोये होते हैं, अपने मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को इतना उज्ज्वल बनाया होता है कि किसी समय भी पुनर्जीवन में आंख खोलते ही उनका संस्कार रूप में साथ आया हुआ ज्ञान खुल खिलाकर उनके आदर्श-व्यक्तित्व में प्रतिबिम्बत एवं मुखरित हो उठता है। ज्ञान प्राप्ति का प्रारम्भिक चरण शिक्षा ही है। शिक्षा के अभाव में कोई भी व्यक्ति ज्ञानवान् नहीं बन सकता।
जीवन पद्धति को आध्यात्मिक मोड़ दिये बिना आत्मा के विकास की सम्भावनायें उज्ज्वल नहीं हो सकती। जीवन में आध्यात्मिक गुणों का- उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्याय-परता, दयाशीलता आदि को जागृत करने का काम शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञानवान् ही नहीं, शीलवान् बनाकर निरामय मानवता के अलंकरणों द्वारा उसके चरित्र का शृंगार कर देती है। शिक्षा सम्पन्न व्यक्ति ही वह विवेक शिल्प सिद्ध कर सकता है जिसके द्वारा गुण, कर्म एवं स्वभाव को वांछित रूप से गढ़ सकना सम्भव हो सकता है। अशिक्षित व्यक्ति का संपूर्ण जीवन क्या बाह्य और क्या आन्तरिक विकारों एवं विकृतियों से भरा हुआ ऊबड़ खाबड़ बना रहता है। अशिक्षित व्यक्ति न तो जीवन की साज संभालकर सकता है और न उसका उद्देश्य ही समझ सकता है।
अशिक्षित व्यक्ति जब सामान्य जीवन की साधारण परिस्थितियों तक का निर्वाह सफलता एवं कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता जब वह आत्मोद्धार की प्रवीणतापूर्ण प्रयत्नों को किस प्रकार कार्यान्वित कर सकता है। कर्म कुशल वह आध्यात्मिक कर्म-कुशलता केवल शिक्षा के बल पर ही खोजी, पाई और प्रयोग की जा सकती है। जो अशिक्षित व्यक्ति पत्र पढ़वाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जो यह नहीं समझ पाता कि जिस कागज पर उसने अंगूठा छापा है, उसमें क्या लिखा है, जिस मनीआर्डर को वह प्राप्त कर रहा है, उसमें कितने रुपये लिखे हैं। वह भला आत्मिक विकास के सूक्ष्म उपायों को क्या जान सकता है? उसके लिए आत्मा, परमात्मा, प्रकृति पुरुष, मोक्ष मुक्ति, कर्म, अकर्म, पाप पुण्य आदि की परिभाषायें ऐसी अनबूझ ही रहती हैं जैसे किसी बालक के लिये पक्षियों का कलरव वह केवल इतना ही अनुभव कर सकता है, यदि कर सके—यह कुछ है तो अच्छा किन्तु यह नहीं समझ सकता कि इन सबका अर्थ और उद्देश्य क्या है।
पशु क्या है? एक प्राणी। और मनुष्य- वह भी एक प्राणी है। एक चतुष्पद और दूसरा द्विपद। दोनों खाते खेलते और एक से अनेकता सम्पादित करते हैं। दोनों भूख प्यास अनुभव करते हैं और दोनों नींद से निमीलित होते हैं। दोनों स्वार्थ के लिये लड़ते झगड़ते और दोनों ही समान रूप से अपने सामान्य हित-अनहित को जानते हैं। जैसे अन्य पशु-पक्षियों को दुःख सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी। जीवों के असंख्यों आकार प्रकारों में से एक मनुष्याकार भी है। हाथ-पैर, नाक-कान, पेट-पीठ सम्बन्धी कायिक कौतूहल पशु और मनुष्य प्राणी के बीच किसी मूल एवं महत्वपूर्ण भेद की प्रवक्ता नहीं है।
संसार के अन्य प्राणियों से भिन्न मानव-प्राणी मनुष्य की यथार्थक संज्ञा का अधिकारी तब ही बनता है जब वह प्रकृत प्रेरणाओं एवं प्रवृत्तियों का परिष्कार कर आध्यात्मिक आलोक में उनका प्रयोग कर सकने को योग्यता विकसित कर लेता है। अन्यथा, अन्य प्राणियों और मानव प्राणी में कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार जीव जगत् में किसी को गाय, बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, हिरन आदि अभिधानों से सम्बोधित किया जाता है, उसी प्रकार इस दद्विपदगामी मनुष्य को भी नर-पशु नाम से पुकारा जाता है। अन्य जीव-जन्तुओं तथा मनुष्य के बीच जो मूल एवं महत्त्वपूर्ण अन्तर है, वह यह कि मनुष्य ‘आत्म-जीवी’ है, जबकि अन्य जीव ‘शरीर जीवी’ होते हैं। उनकी सारी इच्छायें, अभिलाषायें एवं आवश्यकतायें केवल शरीर तक ही सीमित रहती हैं, जबकि मनुष्य की अभिलाषायें आध्यात्मिक और आवश्यकतायें आत्मिक स्तर तक जा पहुंचती हैं। वह विवेक-बुद्धि अन्य प्राणियों में नहीं होती, जिसके प्रसाद से मनुष्य ने आत्मा को जाना-पहचाना और उसके उद्धार के लिये प्रयत्न पथ का प्रस्तुत किया।
आत्मा की परिचायक इस विवेक बुद्धि का विकास जड़तापूर्ण स्थिति में नहीं हो सकता। इसके लिए मनुष्य को साक्षर ही नहीं, शिक्षित होना होगा। अशिक्षा का अभिशाप पाप की प्रेरणा देकर मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही नष्ट कर देता है। कर्म-अकर्म का ज्ञान न होने से अशिक्षित व्यक्ति की अधिकांश क्रियायें अन्धकार की ओर ही ले जाने वाली सिद्ध होती हैं। जड़ताजन्य प्रेरणाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार तथा ईर्ष्या-द्वेष स्वार्थ, अदय एवं अनधिकारिता का विष व्याप्त रहता है। जिससे मनुष्य की आत्मा प्रबुद्ध होने के स्थान पर अधिकाधिक निश्चेष्ट होती जाती है। अन्धकार में चलने वाला व्यक्ति जिस प्रकार अन्तर में ‘अज्ञान’ का अन्धकार लेकर चलने वाला अशिक्षित व्यक्ति संसार पथ पर अविराम गति से नहीं चल सकता। प्रतिपल, पतन का भय उसे कभी भी आत्मोद्धार की दिशा में बढ़ने देगा, ऐसी आशा कर सकना संभव नहीं।
जो अशिक्षित है, अज्ञानी है और इस अभिशाप को मिटा डालने में रुचि नहीं रखता उसे उस आत्मा का अमित्र ही कहा जायेगा, जो परमात्मा का पावन अंश है। और शरीर साधन को सक्रिय रखने के लिये चेतना रूप से इस उद्देश्य से स्थापित की गई है कि वह उसे जाने और उसके माध्यम से विश्व-ब्रह्माण्ड के कारण भूत परमात्मा को पहचान कर मुक्ति पद का अधिकारी बने।
जो आत्मा की जिज्ञासा नहीं करता और उसे मुक्त करने के प्रयत्नों की ओर से विमुख है, वह जन्म-जन्मान्तरों तक इस प्रकार ही दुःख भोगता रहेगा, जिस प्रकार वर्तमान में भोग रहा है। ज्ञान के अतिरिक्त इस भ्रामक भव रोग की अन्य औषधि नहीं, जिसकी प्राप्ति विद्या बल पर ही की जा सकती है।
लोक की सफलता और परलोक की संराधना के लिये शिक्षितों को ज्ञान और अशिक्षितों को शिक्षा की ओर अग्रसर होना ही चाहिये। परिस्थितिवश जिन्हें शिक्षा का अवसर न हो, वे जिस प्रकार भी हो सके साक्षरता के अक्षत तो डाल ही लें। इससे उनके सूक्ष्म अन्तःकरण में विद्या के बीज पड़ जायेंगे, जोकि संस्कार रूप में उनके साथ जाकर पुनः अथवा पुनरपि जन्म में पुष्पित एवं पल्लवित होकर ही रहेंगे।
शिक्षण का दूसरा क्षेत्र है—आत्म-ज्ञान, धर्म, अध्यात्म। इसे विद्या के नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। शिक्षा और विद्या में मौलिक अन्तर है। शिक्षा उसे कहते हैं जो जीवन के बाह्य प्रयोजनों को पूर्ण करने में सुयोग्य मार्ग दर्शन करती है। साहित्य, शिल्प, कला, विज्ञान, उद्योग, स्वास्थ्य, समाज आदि विषय इसी शिक्षा परिधि में आते हैं। विद्या का क्षेत्र इससे आगे का है—आत्मबोध, आत्म निर्माण, कर्त्तव्य निष्ठा, सदाचरण, समाज निष्ठा आदि वे सभी विषय विद्या कहे जाते हैं जो वैयक्तिक चिन्तन, दृष्टिकोण एवं सम्मान में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता का समावेश करते हों। स्वार्थपरता को घटाने और लोक निष्ठा को बढ़ाते हों। धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा मात्र इसी प्रयोजन के लिए तत्त्वदर्शियों ने खड़ा किया है।
ईश्वर भक्ति, उपासना, योग-साधना, धर्मानुष्ठान, कथा कीर्तन, स्वाध्याय सत्संग, दान, पुण्य आदि का जो जितना कुछ भी धर्म कलेवर खड़ा है, इस सबके पीछे एक ही उद्देश्य है मनुष्य व्यक्तिवादी पशु प्रवृत्तियों से छुटकारा पाये और समाज निष्ठा के परमार्थ मार्ग को अपनाकर उदार एवं लोकसेवी प्रक्रिया अपनाये। इस मूल प्रयोजन की ओर मनुष्य को अग्रगामी बनाने के लिए अनेक कथा पुराण बनाये गये—धर्म शास्त्र रचे गये, साधन विधान बनाये गये—स्वर्ग नरक के भय प्रलोभन प्रस्तुत किये गये। अदृश्य जगत के लोक-लोकान्तरों के देव दानवों के प्रतिपादन किये गये। मत-मतान्तरों के बीच इन प्रतिपादनों में भारी अन्तर पाया जाता है पर मूल प्रयोजन सबका एक है- मनुष्य की पशु प्रवृत्ति को, व्यक्तिवादी स्वार्थपरता को समाज निष्ठ परमार्थ को धर्म धारणा में विकसित करना।
इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र की तरह विद्या क्षेत्र में भी रूढ़िवादिता का साम्राज्य है। धर्म पुरोहित अब केवल आवरण की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और मूल उद्देश्य को भुला रहे हैं। अमुक धर्मानुष्ठान का कर्मकाण्ड पूरा कर देने से, कथा कीर्तन के श्रवण, नदी सरोवर के स्नान, तीर्थ, मन्दिर दर्शन, जप तप मात्र को स्वर्ग मुक्ति का आधार घोषित कर दिया गया है। आन्तिरिक दृष्टि से मनुष्य घोर व्यक्तिवादी, समाज विरोधी रहकर भी इस धर्माचरण की सहायता से सद् गति प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का कृपापात्र बन सकता है। आज इसी प्रतिपादन की धूम है। इसे ज्ञान के नाम पर अज्ञान का प्रसार ही कहना चाहिए। प्राण रहित लाभ की तरह धर्म का आवरण भर खड़ा रखा जा रहा है और यह भुलाया जा रहा है कि यह विशाल आवरण आखिर खड़ा किसलिये किया गया है।
आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के साथ-साथ विद्या के क्षेत्र में भी क्रान्ति उपस्थित की जाय। ढर्रे की शिक्षा भार भूत है। भौतिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता जो शिक्षा हमें प्रदान न कर सके उसे उपयोगी कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार जो विद्या मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता एवं आदर्शवाद का समावेश न करे—व्यक्तिवादी स्वार्थपरता से विरत कर समूहवादी परमार्थ में संलग्न न करे—उसे भी भार भूत ही कहना चाहिए। इस निष्प्राण धर्म कलेवर से केवल धर्म व्यवसायियों का लाभ हो सकता है। जन साधारण को तो उलटे अज्ञान में भटकते हुए अपने धन और समय की बर्बादी का घाटा ही उठाना पड़ेगा। विद्या क्षेत्र की इस विडम्बना का भी अब अन्त ही किया जाना चाहिए। दिवा स्वप्नों में भटकने भटकाने की प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।
आत्म विद्या का-धर्म धारणा का स्वरूप सार्थक और सोद्देश्य होना चाहिए। कथा पुराण एवं धर्मानुष्ठान भले ही किसी रूप में हों पर उनका लक्ष्य उतने भर से आत्म-लाभ मिल जाने के प्रतिपादन से ऊंचा उठकर यह रहना चाहिए कि विश्व मानव को भगवान मानकर उसकी स्थिति ऊंची उठाने में योगदान देकर सच्ची भक्ति भावना का परिचय दिया जाय। प्रेरणा युक्त धर्म कलेवर की उपयोगिता ही मानवीय विवेक को स्वीकार हो सकती है। अनास्था के वातावरण को बदलकर आस्तिकता की ओर जन मानस को तभी मोड़ा जा सकता है जब आत्म विद्या का—धर्म धारणा का स्वरूप रूढ़िवादी न रहकर मनुष्य के आन्तरिक उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हो सके। चिर अतीत में तत्व दर्शियों ने इस समस्त प्रक्रिया का सृजन इसी प्रयोजन के लिए किया था, बहुत भटक लेने के बाद अब हमें बदलना चाहिए और धर्म धारणा को परमार्थ प्रयोजन पर केन्द्रित करना चाहिए। धर्म के आधार पर विकसित होने वाली परमार्थ प्रवृत्ति को लोक मंगल में नियोजित करना आत्म-विद्या का मूलभूत प्रयोजन है। उसे इन दिनों पूरी तत्परता के साथ इसी भूल सुधार में लगना चाहिए। पिछले दिनों के भटकाव को सुधारना ही इन दिनों धर्म क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित्य होगा। खोई हुई आस्था और प्रतिष्ठा को वह इसी आधार पर पुनः वापिस लाने में समर्थ होगा।
जिन्हें सचमुच विद्या से प्रेम है उन्हें वर्तमान धर्म शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए आगे आना चाहिए। बुद्धि, प्रतिभा, समय, श्रम और धन का जो जितना बड़ा अंश लोक मंगल के लिए नियोजित कर सके। उसे उतना ही बड़ा धर्मात्मा माना जाय। पिछले अन्धकार युग की सामाजिक एवं बौद्धिक विकृतियां इतनी अधिक अभी भी भरी हुई हैं कि उनकी सफाई में भारी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्शवादी कर्तृत्व को जन साधारण के दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में ध्यान दिलाने के लिए घनघोर प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्रत्येक धर्म प्रेमी को सामयिक कर्त्तव्य समझ कर सर्वतो भावेन संलग्न होना चाहिए। धर्म शिक्षा का, आत्म विद्या का प्रशिक्षण इन दिनों इसी केन्द्र पर केन्द्रित रहना चाहिए। इसी प्रयास को आत्म-कल्याण स्वर्ग-मुक्ति एवं ईश्वर प्राप्ति की सर्वोत्तम युग साधना बनाया जाना चाहिए। धर्म और ईश्वर के नाम पर खर्च होने वाला प्रत्येक पैसा और समय का प्रत्येक क्षण इसी केन्द्र पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।
वानप्रस्थ परम्परा इसीलिए थी कि अधेड़ होने तक मनुष्य अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो ले और जीवन का उत्तरार्ध लोक मंगल के लिए उत्सर्ग करे। इस परम्परा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि सुयोग्य, अवैतनिक, भावनाशील, अनुभवी सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की सेना का उद्भव फिर शुरू हो जाये और उसके द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्रान्ति की—सर्वतोमुखी नव निर्माण की आवश्यकता को पूरा किया जाना सहज ही संभव हो सके है। शिक्षा और विद्या में परिवर्तन और सुधार ही मानवीय प्रगति का मूल भूत आधार है विश्व कल्याण और विश्व शान्ति की उभयपक्षीय प्रयोजन शिक्षा और विद्या के परिष्कार पर अवलम्बित हैं। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाय उतना ही उत्तम।
शिक्षा हमें विद्योपार्जन के योग्य बनाती है। व्यक्तित्व—विकास का वह प्राथमिक सोपान है। विद्या का उद्देश्य सूक्ष्म जगत में प्रवेश की उसकी अनुभूति—सम्वेदना की सामर्थ्य उत्पन्न करना है। शिक्षा स्थूल जगत के व्यावहारिक क्रियाकलापों की विधि सिखाती है। विद्या सूक्ष्म जगत के भावनात्मक विस्तार का परिचय कराती और आस्थाओं को उत्कृष्ट परिपक्व बनाती है। शिक्षा पदार्थ से सम्बन्धित जानकारी देती है विद्या चेतना की अनुभूति एवं में ज्ञान में समर्थ बनाती है। शिक्षा का क्षेत्र है भौतिक जगत विद्या का क्षेत्र इस भौतिक जगत से परे का कोई रहस्यमय संसार नहीं, इसी भौतिक जगत के अन्तराल में निरन्तर क्रियाशील सूक्ष्म जगत है जो चेतना, भावना एवं आस्था द्वारा ही श्रेय है।
सूक्ष्म जगत के जीवन पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों में सी.डब्ल्यू. लैड वीटर की ‘दि अदर साइड ऑफ डैथ’ और श्रीमती ऐनी बेसेन्ट की ‘लाइफ आफ्टर डैथ’ अधिक प्रख्यात है। उन्होंने भौतिक जगत के अन्तराल में विद्यमान सूक्ष्म लोक के अस्तित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है और कहा है कि आत्माएं सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार निवास करती हैं जैसे कि हम लोग स्थूल शरीर से इस प्रत्यक्ष संसार में जीवनयापन करते हैं। मैडम ब्लावटस्की कर्नल आल्काट आदि ने इस सन्दर्भ में अपनी मान्यताओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है।
सात लोकों की तरह आत्मा के भी सात शरीर हैं। स्थूल शरीर को क्रिया लोक कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को विचार लोक और कारण शरीर को भावना लोक। यह मोटी तीन परतें हैं, पर यदि इनका बारीकी से विश्लेषण किया जाय तो वे तीन न रहकर सात हो जाती हैं इनके विभिन्न नाम हैं। इनमें से प्रत्येक परत अधिक शक्तिशाली और अधिक संवेदनशील है। हम स्थूल से सूक्ष्म की परतों में जितना अधिक प्रवेश करते हैं उतना ही अधिक गहरी सशक्तता का समुद्र लहलहाता दीखता है। चेतना के विकास का लक्षण यही है कि ससीम से आगे बढ़कर असीम में प्रवेश करें। चिन्तन की दृष्टि से इसे आत्म-विस्तार कह सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थ परता की परिधि तोड़ कर ‘‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’’ की मान्यता बना लेने वालों का आचरण विश्व नागरिक जैसा होता है और वे परमार्थ प्रयोजनों को ही वास्तविक स्वार्थ साधन मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से ओत-प्रोत होकर वे अपना क्रिया—कलाप इस स्तर का बनाते हैं। जिसके आधार पर लोक-मंगल के महान् प्रयोजनों में अपनी क्षमता संलग्न रह सके। यह आत्म—विकास या आत्म विस्तार हुआ। आध्यात्मवादी इसी दिशा में प्रयत्नशील रहते और आगे बढ़ते हैं।
बात जानने तक ही सीमित नहीं है। सूक्ष्म प्रकृति पर जितनी मात्रा में आधिपत्य होता जाता है। उसी अनुपात से उसकी विचित्र शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार भी मिल जाता है। जिस प्रकार स्थूल सम्पत्ति का लाभ किसी दूसरे को दिया जा सकता है उसी प्रकार सूक्ष्म जगत विभूतियों से भी अपने प्रिय पात्रों को लाभान्वित किया जा सकता है। यह सामर्थ्य वरदान की शक्ति कहलाती है। इसी प्रकार कुपित स्थिति में अपनी मानसिक चेतना का प्रहार करके किसी की हानि भी की जा सकती हैं। इसे शाप की शक्ति कहते हैं। अभिशप्त व्यक्तियों अथवा पदार्थों की दुर्गति होने के कितने ही उदाहरण समय-समय पर मिलते रहते हैं।
ब्रह्म चेतना में प्रवेश करके हम उच्चस्तरीय अतिमानवी उत्कृष्ट भाव चिन्तन उपलब्ध कर सकते हैं। इस आधार पर मनुष्य को उन श्रद्धा सम्वेदनाओं का अनुदान मिलता है जिन्हें देव स्तर की कहा जाता है। इस अवतरण में व्यक्ति अधिकाधिक पवित्र एवं सुसंस्कृत बनता जाता है। आत्मीयता का विस्तार होने से संकीर्ण स्वार्थपरता झड़ने लगती है और उसके स्थान पर ‘‘सब को अपने में और अपने को सब में’’ देखने का दृष्टिकोण विकसित होता है। ऐसी स्थिति में दूसरों के दुःखों को बंटा लेने और अपने सुखों को बांट देने की नीति अपनाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। दया, करुणा, उदारता जैसी सद्भावनाएं अन्तःकरण में उपजती हैं और सद्भावनाओं का विस्तार होने, लोक-मंगल के प्रति अधिकाधिक रुचि बढ़ने, परमार्थ परायण सेवा सहकारिता चरितार्थ करने में रस लेने की प्रवृत्ति स्वयंमेव बढ़ती चली जाती है। व्यक्तियों में सहृदयता, सज्जनता, आदर्शवादी चरित्र निष्ठा भरती और बढ़ती चली जाती है।
सत्प्रयोजनों को अपनाने में एकाकी बढ़ चलने का शौर्य साहस विकसित होता है। अनीति अपनाने वाली दुनिया का बहुमत एक ओर और उसको नीति निष्ठा एकाकी अपने स्थान पर अंगद के पैर की तरह अड़ी रह सकती है। अविवेक का अन्धकार उसे प्रभावित नहीं करता। कौन क्या कहता है। उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं होती। ईमान और भगवान का अनुकूल रहना उसे अपने क्रिया-कलाप को अपनाने में पर्याप्त प्रतीत होता है, अन्य लोग समर्थन करते हैं या विरोध इसकी उसे रत्ती भर भी चिन्ता नहीं रहती। ब्रह्मपरायण व्यक्ति की आत्म चेतना में उच्चस्तरीय सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां बढ़ती और भरती चली जाती हैं। अति मानव में यही विशेषताएं होती हैं। देवात्माओं में यही गुण पाये जाते हैं।
मनुष्य अन्य प्राणियों से ऊंचा अपनी शरीर रचना अथवा बुद्धिकौशल के कारण नहीं बना है। उसकी प्रगति का मूल कारण सहकारिता-सद्भावना एवं उदार चरित्र निष्ठा जैसी सद्भावनाओं में सन्निहित है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनके लिए परिवार समाज एवं शासन की संरचना करना संभव हुआ। सामूहिक प्रयत्नों का ही फल है कि शिक्षा, चिकित्सा, व्यवस्था, उत्पादन, व्यवसाय, विज्ञान जैसी उपलब्धियां संभव हो सकीं। पारस्परिक आदान-प्रदान की विशेषता ने पूर्वजों के अनुभवों से अगली पीढ़ियों को लाभान्वित किया है। उपार्जन का लाभ सबने मिल-जुल कर उठाया है। स्वार्थपरता, लिप्सा और उच्छृंखलता को नैतिक अनुशासन के सहारे कुचला और उदार सहकारिता को कष्ट सहकर भी स्वीकार किया है। मानवी प्रगति के यही आधार हैं। ऐसी ही उत्कृष्ट भाव संवेदनाओं को मानवता कहा जाता है।
शरीर, बल और बुद्धि कौशल की दृष्टि से अन्य प्राणी भी अपनी अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त सामर्थ्य सम्पन्न हैं। हाथी ह्वेल और सिंह की तुलना में मनुष्य का शरीर बल तुच्छ है। हिंस्र पशुओं की आक्रमण चतुरता और शाकाहारियों की आत्म रक्षण कुशलता के दांव पेचों को देखकर लगता है उस क्षेत्र में उनका बुद्धि वैभव मनुष्य से पीछे नहीं आगे ही है। ऋतु प्रभावों एवं क्षुधा, पिपासा जैसी शारीरिक आवश्यकताओं को सहन करने की तितीक्षा शक्ति अपेक्षाकृत पशुओं में अधिक है। बन्दर की तरह पेड़ पर चढ़ना— हिरन की तरह कुलाँच भरना— पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना, मनुष्य से कहां बन पड़ता है। चींटी, दीमक, मकड़ी, मधुमक्खी जैसे छोटे-कीड़ों में ऐसी कितनी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। जो मनुष्य को शायद कभी भी उपलब्ध न हो सकेंगी। कितने ही पक्षी अपने नियत समय पर हजारों मील लम्बी यात्राओं पर निकलते हैं और बिना राह भूले अभीष्ट स्थानों पर प्रवास की अवधि पूरी करके अपने पूर्व स्थानों पर वापिस आ जाते हैं। मनुष्य इन विशेषताओं की दृष्टि से काफी पीछे है। फिर अन्य प्राणी क्यों प्रगति पथ पर आगे न बढ़ सके और मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि कैसे बन गया? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है- उसकी सद्भाव सम्पन्नता आत्मिक उत्कृष्टता।
अध्यात्म विज्ञान का—ब्रह्मविद्या का—एक मात्र लक्ष्य इस सद्भाव सम्पदा की मात्रा बढ़ाते चलना है। ईश्वर का अधिकाधिक सघन सम्पर्क इसी प्रयोजन के लिए अभीष्ट होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जाने वाली विभिन्न साधनाएं किस मात्रा में सफल हो रही हैं इसकी एक मात्र कसौटी यही है कि उस व्यक्ति के अन्तःकरण में निर्मलता एवं कोमल संवेदनाओं का परिमाण कितना बढ़ा, यदि भीतर स्वार्थपरता और निष्ठुरता यथावत बनी रहे तो समझना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किये जाने वाले साधनात्मक प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला। मनुष्य की श्रेष्ठता का यदि आधार ढूंढ़ा जाय तो वह उसकी उन प्रदीप्त सद्भावनाओं में ही देखा जा सकता है जो अपनी प्रखरता के कारण सत्प्रवृत्तियों में परिणत हुए बिना रह ही नहीं सकती। ब्रह्म के असंख्य क्रिया-कलाप हैं पर जब परमात्म चेतना का आत्म चेतना के साथ सम्बन्ध होता है तो बिजली के दोनों तार छूने पर चिनगारियां निकलने की तरह श्रेष्ठता के ही लक्षण प्रकट होते हैं। जिन्हें उत्कृष्ट आदर्शवादिता कहा जाता है। पशु और मनुष्य के बीच इसी विशेषता के अभिवर्धन का अन्तर होता है। इसे अतिरिक्त ईश्वरी अनुग्रह या अनुदान कह सकते हैं।
बुद्धि कौशल ने सद्भावों को बढ़ाया या सद्भावों से बुद्धि कौशल बढ़ा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ते समय बुद्धि चमत्कार का पक्ष लेने को जी करता है क्योंकि प्रत्यक्ष उपयोग उसी का अधिक होता है। सुविधा साधनों के उपार्जन अभिवर्धन में बुद्धि ही अग्रिम मोर्चे पर खड़ी दीखती है इसलिए उसको प्रमुखता दी जाय ऐसा जी करता है किन्तु अधिक गम्भीरता से चिन्तन करने पर तथ्य सर्वथा उलट जाते हैं। जितनी गहराई से उतरते हैं उतनी ही यह सच्चाई सामने आती है। कि मनुष्य की मौलिक विशेषता सद्भावना है इसीलिए उसकी इस प्रधानता-महत्ता को मनुष्यता का नाम दिया जाता रहा है।
सच्चे ब्रह्म परायण व्यक्ति की सत्ता सन्त—सज्जन—परमार्थ परायण, ब्राह्मण, आदर्श के मूर्तिमान प्रतीक ऋषि, युग साधना में निरत महामानव लोक मंगल के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले भूसुर के रूप में अपनी प्रखर उत्कृष्टता का परिचय देती है। विडम्बना रचने वाले और भ्रम जंजालों में उलझे रहने वालों की बात दूसरी है, वे चित्र-विचित्र कर्मकाण्डों में स्तवन उपहारों से ईश्वर को प्रसन्न करने और उससे तरह-तरह की मनोकामनाएं पूरी कराने के ताने-बाने बुनते रहते हैं। इन दिनों अन्य क्षेत्रों में फैले हुए बुद्धि विभ्रम की तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी ऐसी ही विडम्बना चरम सीमा पर पहुंची हुई है और लोग ईश्वर को अपनी चाल बाजियों से फुसला लेने के लिए नित-नये जाल बुनते रहते हैं। इस बाल-बुद्धि से किसे कितना प्रतिफल मिलता है। इसे तो वे ही जानें, पर तथ्य यह है कि यथार्थवादी ईश्वर भक्ति का परिणाम एक ही है अन्तःकरण की सद्भाव सम्पदा का अधिकाधिक विस्तार और परिष्कार। यह वैभव जिन्हें भी प्राप्त होता है वे देव मानव होकर जीते हैं। अपने समीपवर्ती वातावरण में स्वर्ग तुल्य सुख-शांति से घिरा-हरा−भरा बनाते हैं। स्वयं असीम आत्मसंतोष और सघन जन सम्मान प्राप्त करते हैं। समस्त विश्व उनकी कृतियों का कृतज्ञ रहता है। जन-मानस को उनके द्वारा प्रबल प्रेरणा होती है और सामाजिक विकृतियों के समाधान में वे आशातीत योगदान देते हैं। जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाने का यही सफल साधना है। ऐसे व्यक्तियों की चेतना मल आवरण विक्षेपों से रहित होकर जो निर्मलता प्राप्त करती है उससे ब्रह्म चेतना की यथेष्ट मात्रा अपने में धारण कर लेना सम्भव जाता है। इस सम्पदा का परिचय देवात्माओं के ऐसे महान् कृत्यों द्वारा मिलता है जिन्हें सामान्य स्तर से व्यक्ति असामान्य, असम्भव और चमत्कारी मानते हैं। कभी कभी वे भौतिक क्षेत्र में भी अपनी विशिष्टता के ऐसे परिचय देते हैं जिन्हें ऋद्धि-सिद्धि की विशिष्टता कहा जा सके।
अन्तरात्मा में बढ़ती हुई विवेकशीलता जब दूरदर्शिता अपनाने और दृष्टिकोण को परिष्कृत करने में सफल होने लगे तो जानना चाहिए ब्रह्म चेतना का अवतरण हो रहा है। और मनुष्य आत्मिक प्रगति की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा, आकांक्षाएं, वासना, तृष्णा की क्षुद्रता से ऊपर उठती ही हैं। उन्हें लोभ मोह की कीचड़ में सड़ते रहने की दयनीय दुर्दशा असह्य हो उठती है। पेट और प्रजनन तक जीवन सम्पदा को नियोजित किये रहने में उन्हें घाटा ही घाटा दीखता है अस्तु वे अपनी गति विधियों का नये सिरे से निर्धारण करते हैं। विश्व मानव की सेवा साधना में ही उन्हें जीवन सम्पदा की सार्थकता दीखती है अस्तु निर्वाह की आवश्यकताओं को सीमित करते हैं। सादगी से रहते हैं। मितव्ययिता बरतते हैं। परिवार के पिछले उत्तरदायित्वों के निर्वाह में ही जब कमी रह जाती है तो नये बच्चे-कच्चे पैदा करते जाने की मूर्खता तो उनसे बन ही नहीं पड़ती। भौतिक ऐषणाओं को निग्रहीत करने के उपरान्त ही इतनी कुछ सामर्थ्य बच सकती है, जिसके सहारे आत्मिक प्रगति के लिए—ईश्वर प्राप्ति के लिए—अनिवार्य रूप में आवश्यक आदर्शवादी परमार्थ परायणता को अपनाया जाना सम्भव हो सके। सच्ची ईश्वर भक्ति इसी प्रकार किसी सच्चे भक्त पर अवतरित होती है और जीवन की दिशा-धारा बदल डालने के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती है।
जीवनधारा को उत्कृष्टता की इस दिशा में मोड़ देना ही विद्या का लक्ष्य है। उसे ही ब्रह्मविद्या या आत्म विज्ञान कहा जाता है।
बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम साधनों में भी सुखी दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि अज्ञानता के दुष्परिणामों से बचे रहते हैं। उनके प्रत्येक कार्य में विवेक होता है, जो कुछ करते हैं उसे पहले भली प्रकार सोच समझ लेते हैं। पूरी तरह विचार करने के बाद किये गये कार्यों में हानि की सम्भावना प्रायः समाप्त हो जाती है और उस कार्य में पड़ने वाली बाधाओं, परेशानियों और मुसीबतों से बचने का रास्ता मिल जाता है। ज्ञान मनुष्य को जीवन का सही रास्ता प्रदर्शित करता है जिससे उसे कठिनाइयां कम होती और सफलतायें अधिक मिलती हैं। कदाचित् परिस्थितिवश कोई विघ्न आ भी जाए तो अपनी दूरदर्शिता के कारण बुद्धिमान व्यक्ति उसे आसानी से हल कर लेते हैं। ओछे कर्म करने वाले लोगों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि ऐसे कार्य वे अधिकांश अज्ञानतावश ही करते हैं। जीवन की सही दिशा निर्माण करने की क्षमता न तो धन में है, न पद में न प्रतिष्ठा में। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया सत्कर्मों से पूरी होती है। सन्मार्ग में भी कोई स्वतः प्रवृत्त होता हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। यह प्रेरणा हमें औरों से मिलती है। दूसरों की अच्छाइयों का अनुकरण करते हुए ही महानता की मंजिल तक पहुंचने का नियम बना हुआ है। ऐसी बुद्धि किसी को मिल जाए तो उसे यही समझना चाहिए कि परमात्मा की उस पर बड़ी कृपा है। ज्ञान से मनुष्य की ऐसी ही धर्म बुद्धि जागृत होती है। इसलिए ज्ञान को परमात्मा का सर्वोत्तम वरदान मानना पड़ता है।
अज्ञानता के दुष्परिणाम से बचने का यह तरीका सबसे अच्छा है कि हम अपनी मानसिक चेष्टाओं को संसार का रहस्य समझने में लगायें। विचार करने की शक्ति हमें इसीलिए मिली है कि हम सृष्टि की वस्तु स्थिति को समझें और इसका लाभ अपने सजातियों को भी दें, किन्तु यह सब कुछ तभी संभव है जब हमारा ज्ञान बढ़े। जब-तक हम ज्ञानवान् नहीं बनते, अज्ञानता का शैतान हमारे पीछे पड़ा रहेगा, ऐसी अवस्था में हमारी मोह-ग्रन्थियां ज्यों की त्यों बंधी रहेंगी। अज्ञानता का अंधकार और विश्व-रहस्य की जानकारी के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसी से भव-बन्धन टूटते हैं।
व्यक्ति के पात्रत्व की सच्ची कसौटी उसके ज्ञान से होती है। समाज में अधिक देर तक सम्मान व प्रतिष्ठा उन्हीं को मिलती है जो शीलवान, शिष्ट व विनम्र होते हैं। उद्दण्ड दुराचारी व अशिष्ट व्यक्तियों को सभी जगह तिरस्कार ही मिलता है। इन आध्यात्मिक सद्गुणों का आन्तिरिक प्रतिष्ठान ज्ञान से होता है इससे सदाचार में रुचि बढ़ती है। आप्त वचन है ‘‘विद्या ददाति विनयमं, विनयमं ददाति पात्रताम्’’ अर्थात् विद्या से ज्ञान से विनयशीलता आती है। विनयशील ही पात्रत्व के सच्चे अधिकारी होते हैं। मानवीय प्रतिभा का विकास ज्ञान से होता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के महान् व्यक्तित्व का विकास ज्ञान से हुआ है। भगवान् राम, कृष्ण, गौतमबुद्ध, ईसामसीह, सुकरात आदि सभी महापुरुषों ने ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। सांसारिक दुःखों से परित्राण पाने के लिए मानव जाति को सदैव ही इसकी आवश्यकता हुई है। शास्त्रकार ने ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखा है—
मोक्षस्य न हि वासेस्ति न ग्रामान्तर मेव वा। अज्ञान हृदयग्रन्थिर्नाशो मोक्ष इति स्मृत॥ (शिव-गीता)
अर्थात् मोक्ष किसी स्थान विशेष में उपलब्ध नहीं होता। इसे पाने के लिए गांव-गांव भटकने की भी आवश्यकता नहीं। हृदय की अज्ञान ग्रन्थि का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग, मुक्ति का साधन है—ज्ञान। इसे पा लिया तो इसी जीवन में जीवन-मुक्ति मिल गयी समझनी चाहिए।
इस युग में विज्ञान की शाखा प्रशाखायें सर्वत्र फैली हैं। प्रकाश, ताप, स्वर, विद्युत चुम्बकत्व और पदार्थों की जितनी वैज्ञानिक शोध इस युग में हुई है उसी को ज्ञान मानने की आज परम्परा चल पड़ी है। इसी के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन भी हो रहा है। तथाकथित विज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल सभी कर रहे हैं किन्तु यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि ज्ञान, बुद्धि की उस सूक्ष्म क्रियाशीलता का नाम है जो मनुष्य को सन्मार्ग की दिशा में प्रेरित करती है। विज्ञान का फल है इहलौकिक कामना पूर्ति और ज्ञान का सम्बन्ध है अन्तर्जगत से। ज्ञान वह है जो मनुष्य को आत्म-दर्शन में लगाये।
इसके लिए प्रमाद को त्याग कर विनम्र बनना पड़ता है। जो केवल अपनी अहंता प्रतिपादित करते रहते हैं, जिन्हें केवल अहंकार प्यारा है वे अपने संकुचित दृष्टिकोण के कारण ज्ञान के आनन्द और अनुभूति को जान नहीं पाते। छोटे से छोटा बन जाने पर ही महानता की पहचान की जा सकती है। गल्ले के भारी ढेर पंसेरियों में तौले जाते हैं। कपड़ों के थान गजों से नापते हैं। अमुक स्थान कितनी दूर है, यह मील के पत्थर बताते हैं। ऐसे ही विराट के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए महानता के गठबन्धन करने के लिए— हमें विनम्र बनना पड़ता है। भय, लज्जा और संकोच को त्यागकर तत्परतापूर्वक अपनी चेष्टाओं को उस ओर मोड़ना पड़ता है। तब कहीं ज्ञानवान् बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
अपने पास धन हो तो संसार की अनेकों वस्तुएं क्रय की जा सकती हैं। शारीरिक शक्ति हो तो दूसरों पर रौब जमाया जा सकता है। इससे दूसरों पर शासन भी कर सकते हैं औरों के अधिकारों का अपहरण भी कोई बलशाली कर सकता है। किन्तु विद्या किसी से खरीदी नहीं जा सकती दूसरों से छीन भी नहीं सकते। इसके लिए एकान्त में रहकर निरन्तर शोध, अध्ययन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अपनी मानसिक चेष्टाओं को सरस व मनोरंजक कार्यक्रमों से मोड़कर इसमें लगाना पड़ता है। ज्ञानार्जन एक महान् तप है। इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ता, मनस्विता और अध्ययन शीलता अपेक्षित हैं। इसे प्राप्त करने के बाद खो जाने का भय नहीं रहता। किन्हीं बालकों में किशोरावस्था में ही अलौकिक क्षमता या प्रतिभा देखते हैं तो यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि एक ही वय, स्थान व वातावरण में अनुकूल स्थिति प्राप्त होने पर भी दो बालकों की मानसिक शक्ति में यह अन्तर क्यों होता है? तब यह मानना पड़ता है कि एक में पूर्व जन्मों के ज्ञान के संस्कार प्रबल होते हैं दूसरे में क्षीण। भरत, ध्रुव, प्रह्लाद, अभिमन्यु आदि में जन्म से ही प्रखर ज्ञान के उज्ज्वल संस्कार पड़े थे। जगद्गुरु शंकराचार्य ने थोड़ी ही अवस्था में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। यह उनके पिछले जन्मों के परिपक्व ज्ञान के कारण ही हुआ मानना पड़ता है। इससे इस मत की पुष्टि होती है कि चिर-सहयोगी के रूप में जन्म-जन्मान्तरों तक साथ रहने वाला अपना ज्ञान ही है। ज्ञान का नाश नहीं होता। वह अजर है अमर है।
सार्थक जीवन की आधार-शिला ज्ञान है। बुद्धिमत्ता की सच्ची कसौटी यह है कि मनुष्य अपनी सच्ची जीवन दिशा निर्धारित करे। कुछ न कुछ करते रहें चाहें वह अहितकर ही क्यों न हो, यह बात तर्क-संगत प्रतीत नहीं होती। कर्म का महत्व तब है जब उससे हमें अपना जीवन-लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन में सन्मार्ग पर चलने से पूरी होती है। और सन्मार्ग पर देर तक टिके रहना ज्ञान-प्राप्ति से ही सम्भव है। ज्ञान ही इस संसार की सर्वोपरि सम्पत्ति है।
आत्मिक प्रगति के लिए-उत्कृष्ट शिक्षा की आवश्यकता
हमारे जीवन-यापन की क्रियाओं में पाप का पुट प्रवेश न करने पावे- इस सावधानी के लिये ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है। ज्ञान से दृष्टिकोण परिमार्जित होता है, विचार-शक्ति बढ़ती है और युक्तायुक्त निर्णय की क्षमता प्राप्त होती है। क्या पाप है, क्या पाप नहीं है, इसका ज्ञान जीवन एवं कर्म-दर्शन सम्बन्धी पुस्तकों से ही प्राप्त हो सकता है—और वे सद् ग्रन्थ हैं वेद-शास्त्र, गीता, उपनिषद्, रामायण आदि आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुस्तकें इन आर्ष ग्रन्थों के अतिरिक्त लौकिक विद्वानों द्वारा लिखा हुआ एक से एक बढ़कर नैतिक साहित्य भरा पड़ा है—योग्यता तथा युग के अनुसार उसका लाभ भी उठाया जा सकता है।
ज्ञान-गुण प्राप्त करने के लिये जिस वस्तु की प्रथम एवं प्रमुख आवश्यकता है, वह है—शिक्षा। शिक्षा ज्ञान की आधार भूमि है। जो अशिक्षित है, पढ़ा-लिखा नहीं है, वह किसी भी जीवन अथवा कर्म-दर्शन सम्बन्धी पुस्तक का अध्ययन किस प्रकार कर सकता है, किस प्रकार उनकी शिक्षाओं को समझ सकता है और किस प्रकार हृदयंगम कर सकता है? उसके लिये तो ज्ञान से भरी पुस्तकें भी रद्दी कागज से अधिक कोई मूल्य न रखेंगी।
अनेक लोग कबीर दादू, नानक, तुकाराम, रैदास, नरसी यहां तक कि सुकरात, मुहम्मद और ईसा जैसे महात्माओं एवं महापुरुषों का उदाहरण देकर कह सकते हैं कि यह लोग शिक्षित न होने पर भी पूर्ण ज्ञानवान् तथा आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। इनका सम्पूर्ण जीवन आजीवन निष्पाप रहा और निश्चय ही उन्होंने आत्मा को बन्धन मुक्त कर मोक्ष पद पाया है। इससे सिद्ध होता है कि निष्पाप जीवन की सिद्धि के लिये शिक्षा अनिवार्य नहीं है। ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि अनायास ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष अपने पूर्वजन्म के संस्कार साथ लेकर आते हैं।
एक ही शरीर में जीवन की इतिश्री नहीं हो जाती। इसका क्रम जन्म-जन्मान्तरों तक चला करता है और तब तक चलता रहता है, जब तक जीवात्मा पूर्ण निष्पाप होकर मुक्त नहीं हो जाती। अनायास ज्ञानज्ञों का उदाहरण देने वालों को विश्वास रखना चाहिए कि उक्त महात्माओं ने अपने पूर्वजन्मों में ज्ञान पाने के लिये अनर्थक पुरुषार्थ किया होता है। उसके इतने अनुपम एवं उर्वर बीज बोये होते हैं, अपने मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को इतना उज्ज्वल बनाया होता है कि किसी समय भी पुनर्जीवन में आंख खोलते ही उनका संस्कार रूप में साथ आया हुआ ज्ञान खुल खिलाकर उनके आदर्श-व्यक्तित्व में प्रतिबिम्बत एवं मुखरित हो उठता है। ज्ञान प्राप्ति का प्रारम्भिक चरण शिक्षा ही है। शिक्षा के अभाव में कोई भी व्यक्ति ज्ञानवान् नहीं बन सकता।
जीवन पद्धति को आध्यात्मिक मोड़ दिये बिना आत्मा के विकास की सम्भावनायें उज्ज्वल नहीं हो सकती। जीवन में आध्यात्मिक गुणों का- उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्याय-परता, दयाशीलता आदि को जागृत करने का काम शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञानवान् ही नहीं, शीलवान् बनाकर निरामय मानवता के अलंकरणों द्वारा उसके चरित्र का शृंगार कर देती है। शिक्षा सम्पन्न व्यक्ति ही वह विवेक शिल्प सिद्ध कर सकता है जिसके द्वारा गुण, कर्म एवं स्वभाव को वांछित रूप से गढ़ सकना सम्भव हो सकता है। अशिक्षित व्यक्ति का संपूर्ण जीवन क्या बाह्य और क्या आन्तरिक विकारों एवं विकृतियों से भरा हुआ ऊबड़ खाबड़ बना रहता है। अशिक्षित व्यक्ति न तो जीवन की साज संभालकर सकता है और न उसका उद्देश्य ही समझ सकता है।
अशिक्षित व्यक्ति जब सामान्य जीवन की साधारण परिस्थितियों तक का निर्वाह सफलता एवं कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता जब वह आत्मोद्धार की प्रवीणतापूर्ण प्रयत्नों को किस प्रकार कार्यान्वित कर सकता है। कर्म कुशल वह आध्यात्मिक कर्म-कुशलता केवल शिक्षा के बल पर ही खोजी, पाई और प्रयोग की जा सकती है। जो अशिक्षित व्यक्ति पत्र पढ़वाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जो यह नहीं समझ पाता कि जिस कागज पर उसने अंगूठा छापा है, उसमें क्या लिखा है, जिस मनीआर्डर को वह प्राप्त कर रहा है, उसमें कितने रुपये लिखे हैं। वह भला आत्मिक विकास के सूक्ष्म उपायों को क्या जान सकता है? उसके लिए आत्मा, परमात्मा, प्रकृति पुरुष, मोक्ष मुक्ति, कर्म, अकर्म, पाप पुण्य आदि की परिभाषायें ऐसी अनबूझ ही रहती हैं जैसे किसी बालक के लिये पक्षियों का कलरव वह केवल इतना ही अनुभव कर सकता है, यदि कर सके—यह कुछ है तो अच्छा किन्तु यह नहीं समझ सकता कि इन सबका अर्थ और उद्देश्य क्या है।
पशु क्या है? एक प्राणी। और मनुष्य- वह भी एक प्राणी है। एक चतुष्पद और दूसरा द्विपद। दोनों खाते खेलते और एक से अनेकता सम्पादित करते हैं। दोनों भूख प्यास अनुभव करते हैं और दोनों नींद से निमीलित होते हैं। दोनों स्वार्थ के लिये लड़ते झगड़ते और दोनों ही समान रूप से अपने सामान्य हित-अनहित को जानते हैं। जैसे अन्य पशु-पक्षियों को दुःख सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी। जीवों के असंख्यों आकार प्रकारों में से एक मनुष्याकार भी है। हाथ-पैर, नाक-कान, पेट-पीठ सम्बन्धी कायिक कौतूहल पशु और मनुष्य प्राणी के बीच किसी मूल एवं महत्वपूर्ण भेद की प्रवक्ता नहीं है।
संसार के अन्य प्राणियों से भिन्न मानव-प्राणी मनुष्य की यथार्थक संज्ञा का अधिकारी तब ही बनता है जब वह प्रकृत प्रेरणाओं एवं प्रवृत्तियों का परिष्कार कर आध्यात्मिक आलोक में उनका प्रयोग कर सकने को योग्यता विकसित कर लेता है। अन्यथा, अन्य प्राणियों और मानव प्राणी में कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार जीव जगत् में किसी को गाय, बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, हिरन आदि अभिधानों से सम्बोधित किया जाता है, उसी प्रकार इस दद्विपदगामी मनुष्य को भी नर-पशु नाम से पुकारा जाता है। अन्य जीव-जन्तुओं तथा मनुष्य के बीच जो मूल एवं महत्त्वपूर्ण अन्तर है, वह यह कि मनुष्य ‘आत्म-जीवी’ है, जबकि अन्य जीव ‘शरीर जीवी’ होते हैं। उनकी सारी इच्छायें, अभिलाषायें एवं आवश्यकतायें केवल शरीर तक ही सीमित रहती हैं, जबकि मनुष्य की अभिलाषायें आध्यात्मिक और आवश्यकतायें आत्मिक स्तर तक जा पहुंचती हैं। वह विवेक-बुद्धि अन्य प्राणियों में नहीं होती, जिसके प्रसाद से मनुष्य ने आत्मा को जाना-पहचाना और उसके उद्धार के लिये प्रयत्न पथ का प्रस्तुत किया।
आत्मा की परिचायक इस विवेक बुद्धि का विकास जड़तापूर्ण स्थिति में नहीं हो सकता। इसके लिए मनुष्य को साक्षर ही नहीं, शिक्षित होना होगा। अशिक्षा का अभिशाप पाप की प्रेरणा देकर मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही नष्ट कर देता है। कर्म-अकर्म का ज्ञान न होने से अशिक्षित व्यक्ति की अधिकांश क्रियायें अन्धकार की ओर ही ले जाने वाली सिद्ध होती हैं। जड़ताजन्य प्रेरणाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार तथा ईर्ष्या-द्वेष स्वार्थ, अदय एवं अनधिकारिता का विष व्याप्त रहता है। जिससे मनुष्य की आत्मा प्रबुद्ध होने के स्थान पर अधिकाधिक निश्चेष्ट होती जाती है। अन्धकार में चलने वाला व्यक्ति जिस प्रकार अन्तर में ‘अज्ञान’ का अन्धकार लेकर चलने वाला अशिक्षित व्यक्ति संसार पथ पर अविराम गति से नहीं चल सकता। प्रतिपल, पतन का भय उसे कभी भी आत्मोद्धार की दिशा में बढ़ने देगा, ऐसी आशा कर सकना संभव नहीं।
जो अशिक्षित है, अज्ञानी है और इस अभिशाप को मिटा डालने में रुचि नहीं रखता उसे उस आत्मा का अमित्र ही कहा जायेगा, जो परमात्मा का पावन अंश है। और शरीर साधन को सक्रिय रखने के लिये चेतना रूप से इस उद्देश्य से स्थापित की गई है कि वह उसे जाने और उसके माध्यम से विश्व-ब्रह्माण्ड के कारण भूत परमात्मा को पहचान कर मुक्ति पद का अधिकारी बने।
जो आत्मा की जिज्ञासा नहीं करता और उसे मुक्त करने के प्रयत्नों की ओर से विमुख है, वह जन्म-जन्मान्तरों तक इस प्रकार ही दुःख भोगता रहेगा, जिस प्रकार वर्तमान में भोग रहा है। ज्ञान के अतिरिक्त इस भ्रामक भव रोग की अन्य औषधि नहीं, जिसकी प्राप्ति विद्या बल पर ही की जा सकती है।
लोक की सफलता और परलोक की संराधना के लिये शिक्षितों को ज्ञान और अशिक्षितों को शिक्षा की ओर अग्रसर होना ही चाहिये। परिस्थितिवश जिन्हें शिक्षा का अवसर न हो, वे जिस प्रकार भी हो सके साक्षरता के अक्षत तो डाल ही लें। इससे उनके सूक्ष्म अन्तःकरण में विद्या के बीज पड़ जायेंगे, जोकि संस्कार रूप में उनके साथ जाकर पुनः अथवा पुनरपि जन्म में पुष्पित एवं पल्लवित होकर ही रहेंगे।
शिक्षण का दूसरा क्षेत्र है—आत्म-ज्ञान, धर्म, अध्यात्म। इसे विद्या के नाम से सम्बोधित किया जाता रहा है। शिक्षा और विद्या में मौलिक अन्तर है। शिक्षा उसे कहते हैं जो जीवन के बाह्य प्रयोजनों को पूर्ण करने में सुयोग्य मार्ग दर्शन करती है। साहित्य, शिल्प, कला, विज्ञान, उद्योग, स्वास्थ्य, समाज आदि विषय इसी शिक्षा परिधि में आते हैं। विद्या का क्षेत्र इससे आगे का है—आत्मबोध, आत्म निर्माण, कर्त्तव्य निष्ठा, सदाचरण, समाज निष्ठा आदि वे सभी विषय विद्या कहे जाते हैं जो वैयक्तिक चिन्तन, दृष्टिकोण एवं सम्मान में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता का समावेश करते हों। स्वार्थपरता को घटाने और लोक निष्ठा को बढ़ाते हों। धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा मात्र इसी प्रयोजन के लिए तत्त्वदर्शियों ने खड़ा किया है।
ईश्वर भक्ति, उपासना, योग-साधना, धर्मानुष्ठान, कथा कीर्तन, स्वाध्याय सत्संग, दान, पुण्य आदि का जो जितना कुछ भी धर्म कलेवर खड़ा है, इस सबके पीछे एक ही उद्देश्य है मनुष्य व्यक्तिवादी पशु प्रवृत्तियों से छुटकारा पाये और समाज निष्ठा के परमार्थ मार्ग को अपनाकर उदार एवं लोकसेवी प्रक्रिया अपनाये। इस मूल प्रयोजन की ओर मनुष्य को अग्रगामी बनाने के लिए अनेक कथा पुराण बनाये गये—धर्म शास्त्र रचे गये, साधन विधान बनाये गये—स्वर्ग नरक के भय प्रलोभन प्रस्तुत किये गये। अदृश्य जगत के लोक-लोकान्तरों के देव दानवों के प्रतिपादन किये गये। मत-मतान्तरों के बीच इन प्रतिपादनों में भारी अन्तर पाया जाता है पर मूल प्रयोजन सबका एक है- मनुष्य की पशु प्रवृत्ति को, व्यक्तिवादी स्वार्थपरता को समाज निष्ठ परमार्थ को धर्म धारणा में विकसित करना।
इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र की तरह विद्या क्षेत्र में भी रूढ़िवादिता का साम्राज्य है। धर्म पुरोहित अब केवल आवरण की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और मूल उद्देश्य को भुला रहे हैं। अमुक धर्मानुष्ठान का कर्मकाण्ड पूरा कर देने से, कथा कीर्तन के श्रवण, नदी सरोवर के स्नान, तीर्थ, मन्दिर दर्शन, जप तप मात्र को स्वर्ग मुक्ति का आधार घोषित कर दिया गया है। आन्तिरिक दृष्टि से मनुष्य घोर व्यक्तिवादी, समाज विरोधी रहकर भी इस धर्माचरण की सहायता से सद् गति प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का कृपापात्र बन सकता है। आज इसी प्रतिपादन की धूम है। इसे ज्ञान के नाम पर अज्ञान का प्रसार ही कहना चाहिए। प्राण रहित लाभ की तरह धर्म का आवरण भर खड़ा रखा जा रहा है और यह भुलाया जा रहा है कि यह विशाल आवरण आखिर खड़ा किसलिये किया गया है।
आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के साथ-साथ विद्या के क्षेत्र में भी क्रान्ति उपस्थित की जाय। ढर्रे की शिक्षा भार भूत है। भौतिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता जो शिक्षा हमें प्रदान न कर सके उसे उपयोगी कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार जो विद्या मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता एवं आदर्शवाद का समावेश न करे—व्यक्तिवादी स्वार्थपरता से विरत कर समूहवादी परमार्थ में संलग्न न करे—उसे भी भार भूत ही कहना चाहिए। इस निष्प्राण धर्म कलेवर से केवल धर्म व्यवसायियों का लाभ हो सकता है। जन साधारण को तो उलटे अज्ञान में भटकते हुए अपने धन और समय की बर्बादी का घाटा ही उठाना पड़ेगा। विद्या क्षेत्र की इस विडम्बना का भी अब अन्त ही किया जाना चाहिए। दिवा स्वप्नों में भटकने भटकाने की प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।
आत्म विद्या का-धर्म धारणा का स्वरूप सार्थक और सोद्देश्य होना चाहिए। कथा पुराण एवं धर्मानुष्ठान भले ही किसी रूप में हों पर उनका लक्ष्य उतने भर से आत्म-लाभ मिल जाने के प्रतिपादन से ऊंचा उठकर यह रहना चाहिए कि विश्व मानव को भगवान मानकर उसकी स्थिति ऊंची उठाने में योगदान देकर सच्ची भक्ति भावना का परिचय दिया जाय। प्रेरणा युक्त धर्म कलेवर की उपयोगिता ही मानवीय विवेक को स्वीकार हो सकती है। अनास्था के वातावरण को बदलकर आस्तिकता की ओर जन मानस को तभी मोड़ा जा सकता है जब आत्म विद्या का—धर्म धारणा का स्वरूप रूढ़िवादी न रहकर मनुष्य के आन्तरिक उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हो सके। चिर अतीत में तत्व दर्शियों ने इस समस्त प्रक्रिया का सृजन इसी प्रयोजन के लिए किया था, बहुत भटक लेने के बाद अब हमें बदलना चाहिए और धर्म धारणा को परमार्थ प्रयोजन पर केन्द्रित करना चाहिए। धर्म के आधार पर विकसित होने वाली परमार्थ प्रवृत्ति को लोक मंगल में नियोजित करना आत्म-विद्या का मूलभूत प्रयोजन है। उसे इन दिनों पूरी तत्परता के साथ इसी भूल सुधार में लगना चाहिए। पिछले दिनों के भटकाव को सुधारना ही इन दिनों धर्म क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित्य होगा। खोई हुई आस्था और प्रतिष्ठा को वह इसी आधार पर पुनः वापिस लाने में समर्थ होगा।
जिन्हें सचमुच विद्या से प्रेम है उन्हें वर्तमान धर्म शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए आगे आना चाहिए। बुद्धि, प्रतिभा, समय, श्रम और धन का जो जितना बड़ा अंश लोक मंगल के लिए नियोजित कर सके। उसे उतना ही बड़ा धर्मात्मा माना जाय। पिछले अन्धकार युग की सामाजिक एवं बौद्धिक विकृतियां इतनी अधिक अभी भी भरी हुई हैं कि उनकी सफाई में भारी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्शवादी कर्तृत्व को जन साधारण के दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में ध्यान दिलाने के लिए घनघोर प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्रत्येक धर्म प्रेमी को सामयिक कर्त्तव्य समझ कर सर्वतो भावेन संलग्न होना चाहिए। धर्म शिक्षा का, आत्म विद्या का प्रशिक्षण इन दिनों इसी केन्द्र पर केन्द्रित रहना चाहिए। इसी प्रयास को आत्म-कल्याण स्वर्ग-मुक्ति एवं ईश्वर प्राप्ति की सर्वोत्तम युग साधना बनाया जाना चाहिए। धर्म और ईश्वर के नाम पर खर्च होने वाला प्रत्येक पैसा और समय का प्रत्येक क्षण इसी केन्द्र पर केन्द्रित किया जाना चाहिए।
वानप्रस्थ परम्परा इसीलिए थी कि अधेड़ होने तक मनुष्य अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो ले और जीवन का उत्तरार्ध लोक मंगल के लिए उत्सर्ग करे। इस परम्परा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि सुयोग्य, अवैतनिक, भावनाशील, अनुभवी सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की सेना का उद्भव फिर शुरू हो जाये और उसके द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक क्रान्ति की—सर्वतोमुखी नव निर्माण की आवश्यकता को पूरा किया जाना सहज ही संभव हो सके है। शिक्षा और विद्या में परिवर्तन और सुधार ही मानवीय प्रगति का मूल भूत आधार है विश्व कल्याण और विश्व शान्ति की उभयपक्षीय प्रयोजन शिक्षा और विद्या के परिष्कार पर अवलम्बित हैं। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाय उतना ही उत्तम।
शिक्षा हमें विद्योपार्जन के योग्य बनाती है। व्यक्तित्व—विकास का वह प्राथमिक सोपान है। विद्या का उद्देश्य सूक्ष्म जगत में प्रवेश की उसकी अनुभूति—सम्वेदना की सामर्थ्य उत्पन्न करना है। शिक्षा स्थूल जगत के व्यावहारिक क्रियाकलापों की विधि सिखाती है। विद्या सूक्ष्म जगत के भावनात्मक विस्तार का परिचय कराती और आस्थाओं को उत्कृष्ट परिपक्व बनाती है। शिक्षा पदार्थ से सम्बन्धित जानकारी देती है विद्या चेतना की अनुभूति एवं में ज्ञान में समर्थ बनाती है। शिक्षा का क्षेत्र है भौतिक जगत विद्या का क्षेत्र इस भौतिक जगत से परे का कोई रहस्यमय संसार नहीं, इसी भौतिक जगत के अन्तराल में निरन्तर क्रियाशील सूक्ष्म जगत है जो चेतना, भावना एवं आस्था द्वारा ही श्रेय है।
सूक्ष्म जगत के जीवन पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों में सी.डब्ल्यू. लैड वीटर की ‘दि अदर साइड ऑफ डैथ’ और श्रीमती ऐनी बेसेन्ट की ‘लाइफ आफ्टर डैथ’ अधिक प्रख्यात है। उन्होंने भौतिक जगत के अन्तराल में विद्यमान सूक्ष्म लोक के अस्तित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है और कहा है कि आत्माएं सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार निवास करती हैं जैसे कि हम लोग स्थूल शरीर से इस प्रत्यक्ष संसार में जीवनयापन करते हैं। मैडम ब्लावटस्की कर्नल आल्काट आदि ने इस सन्दर्भ में अपनी मान्यताओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है।
सात लोकों की तरह आत्मा के भी सात शरीर हैं। स्थूल शरीर को क्रिया लोक कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को विचार लोक और कारण शरीर को भावना लोक। यह मोटी तीन परतें हैं, पर यदि इनका बारीकी से विश्लेषण किया जाय तो वे तीन न रहकर सात हो जाती हैं इनके विभिन्न नाम हैं। इनमें से प्रत्येक परत अधिक शक्तिशाली और अधिक संवेदनशील है। हम स्थूल से सूक्ष्म की परतों में जितना अधिक प्रवेश करते हैं उतना ही अधिक गहरी सशक्तता का समुद्र लहलहाता दीखता है। चेतना के विकास का लक्षण यही है कि ससीम से आगे बढ़कर असीम में प्रवेश करें। चिन्तन की दृष्टि से इसे आत्म-विस्तार कह सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थ परता की परिधि तोड़ कर ‘‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’’ की मान्यता बना लेने वालों का आचरण विश्व नागरिक जैसा होता है और वे परमार्थ प्रयोजनों को ही वास्तविक स्वार्थ साधन मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से ओत-प्रोत होकर वे अपना क्रिया—कलाप इस स्तर का बनाते हैं। जिसके आधार पर लोक-मंगल के महान् प्रयोजनों में अपनी क्षमता संलग्न रह सके। यह आत्म—विकास या आत्म विस्तार हुआ। आध्यात्मवादी इसी दिशा में प्रयत्नशील रहते और आगे बढ़ते हैं।
बात जानने तक ही सीमित नहीं है। सूक्ष्म प्रकृति पर जितनी मात्रा में आधिपत्य होता जाता है। उसी अनुपात से उसकी विचित्र शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार भी मिल जाता है। जिस प्रकार स्थूल सम्पत्ति का लाभ किसी दूसरे को दिया जा सकता है उसी प्रकार सूक्ष्म जगत विभूतियों से भी अपने प्रिय पात्रों को लाभान्वित किया जा सकता है। यह सामर्थ्य वरदान की शक्ति कहलाती है। इसी प्रकार कुपित स्थिति में अपनी मानसिक चेतना का प्रहार करके किसी की हानि भी की जा सकती हैं। इसे शाप की शक्ति कहते हैं। अभिशप्त व्यक्तियों अथवा पदार्थों की दुर्गति होने के कितने ही उदाहरण समय-समय पर मिलते रहते हैं।
ब्रह्म चेतना में प्रवेश करके हम उच्चस्तरीय अतिमानवी उत्कृष्ट भाव चिन्तन उपलब्ध कर सकते हैं। इस आधार पर मनुष्य को उन श्रद्धा सम्वेदनाओं का अनुदान मिलता है जिन्हें देव स्तर की कहा जाता है। इस अवतरण में व्यक्ति अधिकाधिक पवित्र एवं सुसंस्कृत बनता जाता है। आत्मीयता का विस्तार होने से संकीर्ण स्वार्थपरता झड़ने लगती है और उसके स्थान पर ‘‘सब को अपने में और अपने को सब में’’ देखने का दृष्टिकोण विकसित होता है। ऐसी स्थिति में दूसरों के दुःखों को बंटा लेने और अपने सुखों को बांट देने की नीति अपनाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता। दया, करुणा, उदारता जैसी सद्भावनाएं अन्तःकरण में उपजती हैं और सद्भावनाओं का विस्तार होने, लोक-मंगल के प्रति अधिकाधिक रुचि बढ़ने, परमार्थ परायण सेवा सहकारिता चरितार्थ करने में रस लेने की प्रवृत्ति स्वयंमेव बढ़ती चली जाती है। व्यक्तियों में सहृदयता, सज्जनता, आदर्शवादी चरित्र निष्ठा भरती और बढ़ती चली जाती है।
सत्प्रयोजनों को अपनाने में एकाकी बढ़ चलने का शौर्य साहस विकसित होता है। अनीति अपनाने वाली दुनिया का बहुमत एक ओर और उसको नीति निष्ठा एकाकी अपने स्थान पर अंगद के पैर की तरह अड़ी रह सकती है। अविवेक का अन्धकार उसे प्रभावित नहीं करता। कौन क्या कहता है। उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं होती। ईमान और भगवान का अनुकूल रहना उसे अपने क्रिया-कलाप को अपनाने में पर्याप्त प्रतीत होता है, अन्य लोग समर्थन करते हैं या विरोध इसकी उसे रत्ती भर भी चिन्ता नहीं रहती। ब्रह्मपरायण व्यक्ति की आत्म चेतना में उच्चस्तरीय सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां बढ़ती और भरती चली जाती हैं। अति मानव में यही विशेषताएं होती हैं। देवात्माओं में यही गुण पाये जाते हैं।
मनुष्य अन्य प्राणियों से ऊंचा अपनी शरीर रचना अथवा बुद्धिकौशल के कारण नहीं बना है। उसकी प्रगति का मूल कारण सहकारिता-सद्भावना एवं उदार चरित्र निष्ठा जैसी सद्भावनाओं में सन्निहित है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनके लिए परिवार समाज एवं शासन की संरचना करना संभव हुआ। सामूहिक प्रयत्नों का ही फल है कि शिक्षा, चिकित्सा, व्यवस्था, उत्पादन, व्यवसाय, विज्ञान जैसी उपलब्धियां संभव हो सकीं। पारस्परिक आदान-प्रदान की विशेषता ने पूर्वजों के अनुभवों से अगली पीढ़ियों को लाभान्वित किया है। उपार्जन का लाभ सबने मिल-जुल कर उठाया है। स्वार्थपरता, लिप्सा और उच्छृंखलता को नैतिक अनुशासन के सहारे कुचला और उदार सहकारिता को कष्ट सहकर भी स्वीकार किया है। मानवी प्रगति के यही आधार हैं। ऐसी ही उत्कृष्ट भाव संवेदनाओं को मानवता कहा जाता है।
शरीर, बल और बुद्धि कौशल की दृष्टि से अन्य प्राणी भी अपनी अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त सामर्थ्य सम्पन्न हैं। हाथी ह्वेल और सिंह की तुलना में मनुष्य का शरीर बल तुच्छ है। हिंस्र पशुओं की आक्रमण चतुरता और शाकाहारियों की आत्म रक्षण कुशलता के दांव पेचों को देखकर लगता है उस क्षेत्र में उनका बुद्धि वैभव मनुष्य से पीछे नहीं आगे ही है। ऋतु प्रभावों एवं क्षुधा, पिपासा जैसी शारीरिक आवश्यकताओं को सहन करने की तितीक्षा शक्ति अपेक्षाकृत पशुओं में अधिक है। बन्दर की तरह पेड़ पर चढ़ना— हिरन की तरह कुलाँच भरना— पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना, मनुष्य से कहां बन पड़ता है। चींटी, दीमक, मकड़ी, मधुमक्खी जैसे छोटे-कीड़ों में ऐसी कितनी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। जो मनुष्य को शायद कभी भी उपलब्ध न हो सकेंगी। कितने ही पक्षी अपने नियत समय पर हजारों मील लम्बी यात्राओं पर निकलते हैं और बिना राह भूले अभीष्ट स्थानों पर प्रवास की अवधि पूरी करके अपने पूर्व स्थानों पर वापिस आ जाते हैं। मनुष्य इन विशेषताओं की दृष्टि से काफी पीछे है। फिर अन्य प्राणी क्यों प्रगति पथ पर आगे न बढ़ सके और मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि कैसे बन गया? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है- उसकी सद्भाव सम्पन्नता आत्मिक उत्कृष्टता।
अध्यात्म विज्ञान का—ब्रह्मविद्या का—एक मात्र लक्ष्य इस सद्भाव सम्पदा की मात्रा बढ़ाते चलना है। ईश्वर का अधिकाधिक सघन सम्पर्क इसी प्रयोजन के लिए अभीष्ट होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जाने वाली विभिन्न साधनाएं किस मात्रा में सफल हो रही हैं इसकी एक मात्र कसौटी यही है कि उस व्यक्ति के अन्तःकरण में निर्मलता एवं कोमल संवेदनाओं का परिमाण कितना बढ़ा, यदि भीतर स्वार्थपरता और निष्ठुरता यथावत बनी रहे तो समझना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किये जाने वाले साधनात्मक प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला। मनुष्य की श्रेष्ठता का यदि आधार ढूंढ़ा जाय तो वह उसकी उन प्रदीप्त सद्भावनाओं में ही देखा जा सकता है जो अपनी प्रखरता के कारण सत्प्रवृत्तियों में परिणत हुए बिना रह ही नहीं सकती। ब्रह्म के असंख्य क्रिया-कलाप हैं पर जब परमात्म चेतना का आत्म चेतना के साथ सम्बन्ध होता है तो बिजली के दोनों तार छूने पर चिनगारियां निकलने की तरह श्रेष्ठता के ही लक्षण प्रकट होते हैं। जिन्हें उत्कृष्ट आदर्शवादिता कहा जाता है। पशु और मनुष्य के बीच इसी विशेषता के अभिवर्धन का अन्तर होता है। इसे अतिरिक्त ईश्वरी अनुग्रह या अनुदान कह सकते हैं।
बुद्धि कौशल ने सद्भावों को बढ़ाया या सद्भावों से बुद्धि कौशल बढ़ा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ते समय बुद्धि चमत्कार का पक्ष लेने को जी करता है क्योंकि प्रत्यक्ष उपयोग उसी का अधिक होता है। सुविधा साधनों के उपार्जन अभिवर्धन में बुद्धि ही अग्रिम मोर्चे पर खड़ी दीखती है इसलिए उसको प्रमुखता दी जाय ऐसा जी करता है किन्तु अधिक गम्भीरता से चिन्तन करने पर तथ्य सर्वथा उलट जाते हैं। जितनी गहराई से उतरते हैं उतनी ही यह सच्चाई सामने आती है। कि मनुष्य की मौलिक विशेषता सद्भावना है इसीलिए उसकी इस प्रधानता-महत्ता को मनुष्यता का नाम दिया जाता रहा है।
सच्चे ब्रह्म परायण व्यक्ति की सत्ता सन्त—सज्जन—परमार्थ परायण, ब्राह्मण, आदर्श के मूर्तिमान प्रतीक ऋषि, युग साधना में निरत महामानव लोक मंगल के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले भूसुर के रूप में अपनी प्रखर उत्कृष्टता का परिचय देती है। विडम्बना रचने वाले और भ्रम जंजालों में उलझे रहने वालों की बात दूसरी है, वे चित्र-विचित्र कर्मकाण्डों में स्तवन उपहारों से ईश्वर को प्रसन्न करने और उससे तरह-तरह की मनोकामनाएं पूरी कराने के ताने-बाने बुनते रहते हैं। इन दिनों अन्य क्षेत्रों में फैले हुए बुद्धि विभ्रम की तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी ऐसी ही विडम्बना चरम सीमा पर पहुंची हुई है और लोग ईश्वर को अपनी चाल बाजियों से फुसला लेने के लिए नित-नये जाल बुनते रहते हैं। इस बाल-बुद्धि से किसे कितना प्रतिफल मिलता है। इसे तो वे ही जानें, पर तथ्य यह है कि यथार्थवादी ईश्वर भक्ति का परिणाम एक ही है अन्तःकरण की सद्भाव सम्पदा का अधिकाधिक विस्तार और परिष्कार। यह वैभव जिन्हें भी प्राप्त होता है वे देव मानव होकर जीते हैं। अपने समीपवर्ती वातावरण में स्वर्ग तुल्य सुख-शांति से घिरा-हरा−भरा बनाते हैं। स्वयं असीम आत्मसंतोष और सघन जन सम्मान प्राप्त करते हैं। समस्त विश्व उनकी कृतियों का कृतज्ञ रहता है। जन-मानस को उनके द्वारा प्रबल प्रेरणा होती है और सामाजिक विकृतियों के समाधान में वे आशातीत योगदान देते हैं। जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाने का यही सफल साधना है। ऐसे व्यक्तियों की चेतना मल आवरण विक्षेपों से रहित होकर जो निर्मलता प्राप्त करती है उससे ब्रह्म चेतना की यथेष्ट मात्रा अपने में धारण कर लेना सम्भव जाता है। इस सम्पदा का परिचय देवात्माओं के ऐसे महान् कृत्यों द्वारा मिलता है जिन्हें सामान्य स्तर से व्यक्ति असामान्य, असम्भव और चमत्कारी मानते हैं। कभी कभी वे भौतिक क्षेत्र में भी अपनी विशिष्टता के ऐसे परिचय देते हैं जिन्हें ऋद्धि-सिद्धि की विशिष्टता कहा जा सके।
अन्तरात्मा में बढ़ती हुई विवेकशीलता जब दूरदर्शिता अपनाने और दृष्टिकोण को परिष्कृत करने में सफल होने लगे तो जानना चाहिए ब्रह्म चेतना का अवतरण हो रहा है। और मनुष्य आत्मिक प्रगति की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा, आकांक्षाएं, वासना, तृष्णा की क्षुद्रता से ऊपर उठती ही हैं। उन्हें लोभ मोह की कीचड़ में सड़ते रहने की दयनीय दुर्दशा असह्य हो उठती है। पेट और प्रजनन तक जीवन सम्पदा को नियोजित किये रहने में उन्हें घाटा ही घाटा दीखता है अस्तु वे अपनी गति विधियों का नये सिरे से निर्धारण करते हैं। विश्व मानव की सेवा साधना में ही उन्हें जीवन सम्पदा की सार्थकता दीखती है अस्तु निर्वाह की आवश्यकताओं को सीमित करते हैं। सादगी से रहते हैं। मितव्ययिता बरतते हैं। परिवार के पिछले उत्तरदायित्वों के निर्वाह में ही जब कमी रह जाती है तो नये बच्चे-कच्चे पैदा करते जाने की मूर्खता तो उनसे बन ही नहीं पड़ती। भौतिक ऐषणाओं को निग्रहीत करने के उपरान्त ही इतनी कुछ सामर्थ्य बच सकती है, जिसके सहारे आत्मिक प्रगति के लिए—ईश्वर प्राप्ति के लिए—अनिवार्य रूप में आवश्यक आदर्शवादी परमार्थ परायणता को अपनाया जाना सम्भव हो सके। सच्ची ईश्वर भक्ति इसी प्रकार किसी सच्चे भक्त पर अवतरित होती है और जीवन की दिशा-धारा बदल डालने के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती है।
जीवनधारा को उत्कृष्टता की इस दिशा में मोड़ देना ही विद्या का लक्ष्य है। उसे ही ब्रह्मविद्या या आत्म विज्ञान कहा जाता है।