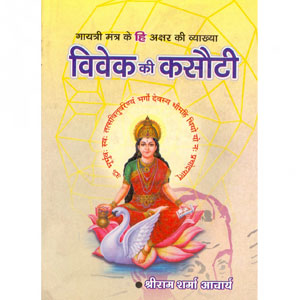विवेक की कसौटी 
विवेक से ही धर्म का निर्णय हो सकता है
Read Scan Version'धर्म' शब्द बड़ा विस्तृत है । अन्य देशीय विद्वानों की बात छोड़ भी दें तो हमारे ही देश के प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों ने धर्म की वह संख्यक व्याख्याएँ की हैं पर अविद्या के कारण आजकल हमारे देश की सामान्य जनता में यह प्रेम फैल गया है कि 'शास्त्र' नाम की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें जो कुछ भी कहा गया है ? लिखा गया है अथवा वर्तमान समय में छाप दिया गया है वह सब कुछ धर्म है पर जैसा हम पहले बता चुके हैं शास्त्रों की रचना भिन्न-भिन्न कालों में परिस्थिति के अनुसार होती रहती है इसलिए उनमें स्वभावत: अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी जान पड़ते वाली बातें पाई जाती हैं । इसके सिवा अनेक विदेशी लोगों ने पिछले डेढ़-दो हजार वर्षों के भीतर गुप्त रूप से अपने मतलब की बातें प्राचीन शास्त्रों में मिला दी हैं । मनुष्यो! इस प्रवृत्ति को समझकर हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट कह दिया था कि धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों के साथ ही अपनी विवेकबुद्धि से स्पष्ट असंगत जान पडे़ वहाँ उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए । मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है और वही सर्वत्र सब पदार्थों और कार्यो में समाया हुआ है । इसलिए मनुष्य यदि आत्मा को निर्मल बनाकर उसकी शक्ति अर्थात विवेक द्वारा विचार करे तो कोई कारण नहीं कि वह सत्य-धर्म का निर्णय न कर सके । उपनिषदों में कहा गया है-
ब्रह्म सर्वमावृत्तय तिष्ठति । ब्रह्मेव सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणि विभर्त्ति । सोऽयमात्मा सर्वानुभूः ।
अर्थात ''सब पदार्थो को घेरकर-लपेटकर, ब्रह्म बैठा है । सब नाम, सब काम, सब रूप उसी एक ब्रह्म के ही 'मैं' हैं । वही आत्मा 'मैं' सब अनुभवों का अनुभव करने वाला है ।''
पुराणों में भी कहा गया है- ससर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व: । -भागवत २. १. ३१ श्रद्धत्स्वानुभूतीऽर्थो न मन: स्प्रष्टुमर्हति । -४. २१. ६५
यस्मिन देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽनुष्ठीयते । स एव देशकालनिमितातरेस्वधर्मो भवति । ।
-शांकर-शारीरिक भाष्य, ३, १, २५
अर्थात ''अधिकारी के भेद से धर्म में भेद होता है । देश, काल, निमित्त के भेद से धर्म में भेद होता है । जिस स्थान पर खड़े होकर देखते हैं, उस स्थान के बदलने से दर्शन अर्थात दृश्य का रूप बदल जाता है । ''जो भी एक देश काल, पात्र, निमित्त और कर्म के विशेष से एक आदमी के लिए धर्म है, वही दूसरे आदमी के लिए दूसरे देश, काल, पात्रता, निमित्त और कर्म के विशेष से अधर्म होता है । केवल एक-दो ग्रंथ पढ़ लेने से धर्म का पता नहीं लगता, अच्छी अवस्था का धर्म दूसरा और विषम अवस्था का धर्म दूसरा होता है ।
बच्चों को मिट्टी का खिलौना ही अच्छा लगेगा, उनको रेखागणित और बीजगणित पड़ाने का यत्न करना व्यर्थ है ।
यही दशा मतों की, संप्रदायों की, पंथों की है । 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना । भिन्नरुचिर्हि लोक: ।'' इत्यादि
अब बचपन बीत जाएगा, तब मिट्टी के खिलौने आप ही छूट जाएँगे और दूसरे प्रकार के खिलौनों में मन लग जाएगा ।
अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम्। बालानां काष्ठ लोष्ठेषु बुधस्यात्मनि देवता । उत्तमा सहजामऽवस्था द्वितीया ध्यान धारणा तृतीया प्रतिमा पूजा, होमयात्रा चतुर्थिका ।
अर्थात ''बालकों के देवता काठ-पत्थर में साधारण मनुष्यों के जल में, मनीषी विद्वानों के आकाश में हैं, बुध का बोध वाले का, ज्ञानवान का देव आत्मा ही है । सहज अवस्था, अर्थात सब दृश्य संसार को ही परमात्मा का स्वरूप जानना, यह उत्तम कोटि है, विशेष ध्यानधारणा करना यह उससे नीची दूसरी कोटि है, प्रतिमाओं की पूजा तीसरी कोटि है, होम और यात्रा चौथी कोटि है ।
बालबुद्धि जीव, जिनकी बुद्धि सर्वथा बहिर्मुख है, जो इंद्रियग्राह्य आकार ही को ग्रहण कर सकते हैं, वे अपने मन का संतोष काष्ठ-लोष्ठ की प्रतिमा से ही करें । यह बहिर्मुख माया रोग मनुष्य का ऐसा बढ़ा हुआ है कि मुसलमान धर्म में भी यद्यपि वह अपने को बड़ा भारी बुतशिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहता है, लोग देवालयों को तोड़कर मकबरे और कब्र बनाते और पूजते हैं । किसी उर्दू शायर ने ही कहा है- जिन्दगाहे तोड़ करके मुर्दगाहें भर दिया ।
इसी बहिर्मुख माया का वर्णन उपनिषदों ने किया है । परांचि खानि व्यतृणत् स्वयंभू: तस्मातं पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिंच्छम् ।।
कठोपनिषद्
अर्थात स्वयंभू ने ब्रह्मा ( श्रृष्ट युन्मुख रज: प्रधान महतत्त्व, बुद्धितत्त्व) ने सब इंद्रियों को, छिद्रों को, बाहर की ओर खोला छेद करके निकाला । इसलिए जीव बाहर की वस्तु देखता है, भीतर अपने को नहीं देखता । कोई-कोई धीर विरक्त जीव संसार की दौड़-धूप, आवागमन और मृत्यु से थककर विश्राम और अमरत्व को चाहकर, आँंख भीतर फेरता है और प्रत्यगात्मा को देखता है ।
पर हाँ उन बालकों के जो रखवारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको यह फिक्र रखनी चाहिए कि बीच-बीच में मिट्टी के खिलौनों के खेल के साथ-साथ कुछ अक्षरज्ञान भी दिखाते जाएँ कुछ पुस्तकों का शौक पैदा कराने का यत्न भी करते रहें । यह न चाहे कि, लड़के सदा खिलौनों में ही खुश रहें, मूर्ख बने रहें, पोथी-पत्रा कभी न छुएँ और हम उनको हमेशा बेवकूफ रखकर अपना गुलाम बनाए रहें ।
और भी यदि ये वृद्ध सात्विक बुद्धि वाले और लोकहितैषी हों तो इस खिलौना पूजा को भी बहुत शिक्षाप्रद उत्तम सात्विक भाववर्द्धक, कलावर्द्धक, शिल्पवर्द्धक शास्त्रप्रवर्तक बना सकते हैं । सुंदर मंदिरों से ग्राम की, नगर की, शोभा-सौंदर्य बढा सकते हैं और उनसे पाठशाला, चिकित्सालय, पुष्पवाटिका, उद्यान चित्रशाला, संगीतादि विविध-कलागृह, सार्वजनिक सभामंडप, सम्मेलन स्थान, व्याख्यानशाला आदि का काम ले सकते । योग साधनादि में भी ये मंदिर सीढ़ी का काम दे सकते हैं । क्योंकि- तच्छृयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते ।
अर्थात ध्यान-धारणा प्राय: किसी मूर्त्त विषय के बिना नहीं सधती । और भी तरह-तरह के उत्तम वैधानिक शास्त्रानुकूल, आधिदैविक शास्त्रसम्मत, आधिभौतिक शास्त्रसम्मत, काम लिए जा सकते हैं । यह याद रखते हुए और यह समझते हुए कि सारा साकार जगत ही उस जगदात्मा का रूप है, जनता को क्रमश: इस मूर्तरूप की ओर ले जाना उचित ही है और इस दृष्टि से मूर्तिपूजा की निंदा करना अनुचित ही है ।
दूसरे दर्जे की बुद्धि के लिए जलमय, तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि की अनुज्ञा दी गई है । अदृष्ट फल वे हैं, जिनसे सूक्ष्मशरीर मनोमय अथवा विज्ञानमय कोश अर्थात अंतःकरण मन, बुद्धि अहंकार का संस्कार हो । दृष्ट फल वे हैं, जिनका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है । इन तीर्थों में भ्रमण करने से देशाटन के जो शिक्षाप्रद बुद्धि की उदारता बढ़ाने वाले, संकोच हटाने वाले, फल हो सकते हैं वे होने चाहिए । यदि तीर्थरक्षक पुजारी और भिखमंगे लोग 'कौआरोड' करके यात्रियों की जान आपत्ति में न डाल दें और तीर्थो के जलों में फल, फूल पत्ता कच्चा और पक्का अन्न डलवा-डलवाकर पानी को सड़ाकर हानिकर न कर डालें । स्वयं पुराणों ने कहा है-
न ह्यम्मयानि तीर्थानि, न देवा मृच्छिलामया । ते पुनंत्युरुकालेन, दर्शनादेव साधव: । ।
-भागवत १० .४८. ३१
अर्थात ''जल में तीर्थ नहीं बनते, न देवता मिट्टी और पत्थर से बनते हैं । उनकी उपासना करने से बहुत काल में मन की शुद्धि होती है, पर सच्चे साधुओं के तो दर्शन और सत्संग से ही चित्त सद्य: शुद्ध हो जाता है । ''तीर्थ- स्थानों में जो सच्चे साधु तपस्वी, विद्वान बसते हैं, वे ही तीर्थ के तीर्थंकर हैं; तीर्थो को तीर्थ बनाने वाले हैं । जो शोक के पार तारे वह तीर्थ ( तरति शोकं येन सहायेन स तीर्थ:) सप्त पवित्र पुरी आदि तीर्थ इसी हेतु से तीर्थ थीं, कि वे उत्तम विद्यापीठ का काम देती थीं । वहाँ की हवा में भक्ति विरक्ति ज्ञान भरा रहता था, क्योंकि इनके बताने और जगाने वाले साधु तपस्वी, विद्वान, पंडित बहुतायत से वहाँ वास करते थे । जैसे आजकल की यूनिवर्सिटियों में किसी एक में एक ही शास्त्र की, किसी दूसरे में दूसरे शास्त्र की विद्या की पढ़ाई, चर्चा, हवा अधिक रहती है, किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी कल-कारखानों की बहुतायतें रहती हैं और वहाँ जाने से उसके संबंध की विद्या सहज ही में आ जाती है । इसी तरह 'काश्यां मरणान् मुक्ति:' काशी में मरने से मुक्ति होती है, क्योंकि वहाँ आत्मज्ञान सहज में साधुओं से मिलना चाहिए चारों ओर उसकी चर्चा होने से मानो हवा में भर रहा है और ''ऋते ज्ञानम् न मुक्ति:'', बिना ज्ञान के छुटकारा नहीं, किसी प्रकार भी गुलामी और बंधन से, सामाजिक से अथवा राजनीतिक से अथवा सांसारिक से, पर आजकल इन पवित्र पुरियों की जो दुर्गति है, वह प्रत्यक्ष है । जो मनुष्य 'काश्या मरणान् मुक्ति:' के अक्षरों को ही पकड़े रहते हैं और उसके हेतु को नहीं पकड़ते और आत्मज्ञान का संचय नहीं करते, उनके लिए मुक्ति की आशा नहीं है ।
तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिए 'दिवि देवा:' सूर्य, बृहस्पति आदि प्रत्यक्ष देवता हैं । इनकी उपासना गणित-फलितात्मक अद्भुत ज्योतिषशास्त्र की उपासना 'मिटियोरोलोजी' आस्ट्रोनोमी ' आदि है । इससे जो कुछ काल-ज्ञान में कृषि में, समुद्र यात्रादि में, सहायता मिल सके वह सब इनकी उपासना का दृष्ट फल है, पर सहायता के स्थान में जो विझ ज्योतिषशास्त्र के कुप्रयोग से ही रहे हैं, वह सबको विदित हैं ।
चौथी और अंतिम कोटि 'बुधस्य आत्मनि देवता' जिसको यह विचार उत्पन्न हो गया है कि यह देवता है या नहीं है, यह पुस्तक मानने योग्य है या नहीं है, यह ऋषिवत् या अवतारवत् या रसूल पैगम्बरवत् या मसीहवत् गुरुवर मानने योग्य है या नहीं है, यह धर्म मानने योग्य है या नहीं है, यह छोड़ने योग्य है या ओढ़ने योग्य है, यह शास्त्र है या अशास्त्र है, यह वेद है या अवेद है, इसका अर्थ यह है या दूसरा है, अंततोगत्वा कोई ईश्वर है या नहीं है और है तो क्या है ? उसका स्वरूप क्या है- इन सबका अंतिम निर्णेता मैं ही हूँ 'मैं' ही है, आत्मा ही है- जिसको यह विचार दृढ हो जाता है, उसके लिए 'बुधस्य आत्मनि देवता' अर्थात बुध का; बुद्धिमान का देव स्वयं आत्मा ही है । परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर 'मैं' ही है । इस काष्ठा को जो पहुँचा है उसके लिए सुरेश्वराचार्य ने वृहदारण्यक वार्तिक में कहा है-' एतांकाष्ठामवष्टभ्यसर्वाम्राह्मणउव्यते । ' जो जीव इस काष्ठा को पहुँचा है, वह ब्राह्मण है और वही ब्राह्मण है अथवा ब्रह्मस्वरूप है ।
उसके लिए 'काश्या मरणान् मुक्ति' की आवश्यकता नहीं किंतु भावना यदि भवेत् फलदात्री मामक नगरमेव हि काशी । व्यापकोऽपि यदि वा परमात्मां तारकं निमिह नोपदिशेन न: ।।
अर्थात भावना ही यदि फल देने वाली है, तो जिस स्थान पर मैं हूँ वही काशी है । यदि परमात्मा व्यापक है, तो यहीं पर तारक यंत्र-मंत्र का उपदेश कर सकता है । ऐसे ही मनुष्य के लिए याज्ञवल्ल स्मृति में कहा है कि वह स्वयं नई आवश्यकता पड़ने पर नया धर्म बना सकता है ।
चत्वारो वेदधूर्मज्ञा: पर्षत्, त्रैविद्यमेव वा । सा ब्रूते यं स धर्म: स्यादेको वाध्यात्मवित्तम ।।
-याज्ञवल्क्य स्मृति १.९
अर्थात ''वेद पर, ज्ञान-समूह पर, प्रतिष्ठापित जो धर्म है, उसके जानने वाले चार मनुष्यों की मंडली अथवा अंगोपांग सहित तीन वेदों को अच्छी तरह जानने वालों की समिति अथवा एक अध्यात्म-वित्तम, ब्रह्मविद्वरिष्ठ, तत्वत: ब्रह्मज्ञान के हृदय में प्रविष्ट, यानी मनुष्य जो निर्णय कर दे कि यह धर्म होना चाहिए वही धर्म माना जाए ।