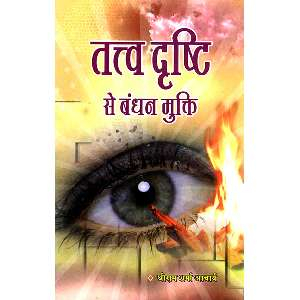तत्वदृष्टि से बंधन मुक्ति 
सुख का केन्द्र और स्रोत आत्मा
Read Scan Version
किसी की यह धारणा सर्वथा मिथ्या है कि सुख का निवास किन्हीं पदार्थों में है। यदि ऐसा रहा होता तो वे सारे पदार्थ जिन्हें सुखदायक माना जाता है, सबको समान रूप से सुखी और सन्तुष्ट रखते अथवा उन पदार्थों के मिल जाने पर मनुष्य सहज ही सुख सम्पन्न हो जाता किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें संसार के वे सारे पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्हें सुख का संराधक माना जाता है। किन्तु ऐसे सम्पन्न व्यक्ति भी असन्तोष, अशान्ति, अतृप्ति अथवा शोक सन्तापों से जलते देखे जाते हैं। उनके उपलब्ध पदार्थ उनका दुःख मिटाने में जरा भी सहायक नहीं हो पाते।
वास्तविक बात यह है कि संसार के सारे पदार्थ जड़ होते हैं। जड़ तो जड़ ही है। उसमें अपनी कोई क्षमता नहीं होती। न तो जड़ पदार्थ किसी को स्वयं सुख दें सकते हैं और न दुःख। क्योंकि उनमें न तो सुखद तत्व होते हैं और न दुःखद तत्व और न उनमें सक्रियता ही होती है, जिससे वे किसी को अपनी विशेषता से प्रभावित कर सकें। यह मनुष्य का अपना आत्म-तत्व ही होता है, जो उससे सम्बन्ध स्थापित करके उसे सुखद या दुःखद बना लेता है। आत्म तत्व की उन्मुखता ही किसी पदार्थ को किसी के लिये सुखद और किसी के लिये दुःखद बना देती है।
जिस समय मनुष्य का आत्म-तत्व सुखोन्मुख होकर पदार्थ से सम्बन्ध स्थापित करता है, वह सुखद बन जाता है और जब आत्मतत्व दुःखोन्मुख होकर सम्बन्ध स्थापित करता है, तब वही पदार्थ उसके लिये दुःखद बन जाता है। संसार के सारे पदार्थ जड़ हैं, वे अपनी ओर से न तो किसी को सुख दें सकते हैं और दुःख। यह मनुष्य का अपना आत्म-तत्व ही होता है, जो सम्बन्धित होकर उनको दुःखदायी अथवा सुखदायी बना देता है। यह धारणा कि सुख की उपलब्धि पदार्थों द्वारा होती है, सर्वथा मिथ्या और अज्ञानपूर्ण है।
किन्तु खेद है कि मनुष्य अज्ञानवश सुख-दुःख के इस रहस्य पर विश्वास नहीं करते और सत्य की खोज संसार के जड़ पदार्थों में किया करते हैं। पदार्थों को सुख का दाता मानकर उन्हें ही संचय करने में अपना बहुमूल्य जीवन बेकार में गंवा देते हैं। केवल इतना ही नहीं कि वे सुख आत्मा में नहीं करते बल्कि पदार्थों के चक्कर में फंसकर उनका संचय करने लिये अकरणीय कार्य तक किया करते हैं। झूंठ, फरेब, मक्कारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के अपराध और पाप तक करने में तत्पर रहते हैं। सुख का निवास पदार्थों में नहीं आत्मा में है। उसे खोजने और पाने के लिये पदार्थों की ओर नहीं आत्मा की ओर उन्मुख होना चाहिए।
पदार्थों का उपभोग इन्द्रियों द्वारा होता है। इन्द्रियों के सक्रिय और सजीव होने से ही किसी रस, सुख अथवा आनन्द की अनुभूति होती है। जब तक मनुष्य सक्षम अथवा युवा बना रहता है, उसकी इन्द्रियां सतेज बनी रहती हैं। पदार्थ और विषयों का आनन्द मिलता रहता है। पर जब मनुष्य वृद्ध अथवा अशक्त हो जाता है—उन्हीं पदार्थों में जिनमें पहले विभोर कर देने वाला आनन्द मिलता था, एकदम नीरस और स्वादहीन लगने लगते हैं। उनका सारा सुख न जाने कहां विलीन हो जाता है। वास्तविक बात यह है कि अशक्तता की दशा अथवा वृद्धावस्था में इन्द्रियां निर्बल तथा अनुभवशीलता से शून्य हो जाती हैं। उनमें किसी पदार्थ का रस लेने की शक्ति नहीं रहती। इन्द्रियों का शैथिल्य ही पदार्थों को नीरस, असुखद तथा निस्सार बना देता है।
वृद्धावस्था ही क्यों? बहुत बार यौवनावस्था में भी सुख की अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। इन्द्रियों में कोई रोग लग जाने अथवा उनको चेतना हीन बना देने वाली कोई घटना घटित हो जाने पर भी उनकी रसानुभूति की शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे रसेन्द्रिय जिह्वा में छाले पड़ जायें तो मनुष्य कितने ही सुस्वाद पदार्थों का सेवन क्यों न करे, उसे उसमें किसी प्रकार का आनन्द न मिलेगा। पाचन क्रिया निर्बल हो जाय तो कोई भी पौष्टिक पदार्थ बेकार हो जायेगा। आंखें विकार युक्त हो जायें तो सुन्दर से सुन्दर दृश्य भी कोई आनन्द नहीं दें पाते। इस प्रकार देख सकते हैं कि सुख पदार्थ में नहीं बल्कि इन्द्रियों की अनुभूति शक्ति में है।
अब देखना यह है कि इन्द्रियों की शक्ति क्या है? बहुत बार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, जिनकी आंखें देखने में सुन्दर स्वच्छ तथा विकार-हीन होती हैं, लेकिन उन्हें दिखलाई नहीं पड़ता। परीक्षा करने पर पता चलता है कि आंखों का यन्त्र भी ठीक है। उनमें आने-जाने वाली नस-नाड़ियों की व्यवस्था भी ठीक है। तथापि दिखलाई नहीं देता। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियां हाथ-पांव, नाक-कान आदि की भी दशा हो जाती है। सब तरफ से सब वस्तुयें ठीक होने पर भी इन्द्रिय निष्क्रिय अथवा निरनुभूति ही रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि रस की अनुभूति इन्द्रियों की स्थूल बनावट से नहीं होती। बल्कि इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है, जो रस की अनुभूति कराती है। वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है चेतना, जो सारे शरीर और मन प्राण में ओत-प्रोत रहकर मनुष्य की इन्द्रियों को रसानुभूति की शक्ति प्रदान करती है। इसी सब ओर से शरीर में ओत-प्रोत चेतना को आत्मा कहते हैं। आनन्द अथवा सुख का निवास आत्मा में ही है। उसी की शक्ति से उसकी अनुभूति होती है और वही जीव रूप में उसका अनुभव भी करती है। सुख न पदार्थों में है और न किसी अन्य वस्तु में। वह आत्मा में ही जीवात्मा द्वारा अनुभव किया जाता है।
मनुष्य की अपनी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा से रहित वह एक मिट्टी का पिण्ड मात्र ही है। शरीर से जब आत्मा का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तो वह मुर्दा हो जाता है। शीघ्र ही उसे बाहर करने और जलाने दफनाने का प्रबन्ध किया जाता है। संसार के सारे सम्बन्ध आत्मा द्वारा ही सम्बन्धित हैं। जब तक जिसमें आत्मभाव बना रहता है, उसमें प्रेम और सुख आदि की अनुभूति बनी रहती है और जब यह आत्मीयता समाप्त हो जाती है वही वस्तु या व्यक्ति अपने लिये कुछ भी नहीं रह जाता। किसी को अपना मित्र बड़ा प्रिय लगता है। उससे मिलने पर हार्दिक आनन्द की उपलब्धि होती है। न मिलने से बेचैनी होती है। किन्तु जब किन्हीं कारणोंवश उससे मैत्री भाव समाप्त हो जाता है अथवा आत्मीयता नहीं रहती तो वह मित्र अपने लिए, एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। उसके मिलने न मिलने में किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं होता। बहुत बार तो उससे इतनी विमुखता हो जाती है कि मिलने अथवा दिखने पर अन्यथा अनुभव होता है। प्रेम, सुख और आनन्द की सारी अनुभूतियां आत्मा से ही सम्बन्धित होती हैं, किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा पदार्थ से नहीं। सुख का संसार आत्मा में ही बसा हुआ है। उसे उसमें खोजना चाहिये। सांसारिक विषयों अथवा वस्तुओं में भटकते रहने से वही दशा और परिणाम सामने आयेगा, जो मरीचिका में भूल मृग के सामने आता है।
मनुष्य की अपनी विशेषता ही उसके लिये उपयोगिता तथा स्नेह सौजन्य उपार्जित करती है। विशेषता समाप्त होते ही मनुष्य का मूल्य भी समाप्त हो जाता है और तब वह न तो किसी के लिये आकर्षक रह जाता है और न प्रिय! इस बात को समझने के लिए सबसे अधिक निकट रहने वाले मां और बच्चे को ले लीजिये। माता से जब तक बच्चा दूध और जीवन रस पाता रहता है, उसके शरीर से अवयव की तरह चिपटा रहता है। उसे मां से असीम प्रेम होता है। जरा देर को भी वह मां से अलग नहीं हो सकता। मां उसे छोड़कर कहीं गई नहीं कि वह रोने लगता है। किन्तु जब इसी बालक को अपनी सुरक्षा तथा जीवन के लिये मां की गोद और दूध की आवश्यकता नहीं रहती अथवा रोग आदि के कारण मां की यह विशेषता समाप्त हो जाती है तो बच्चा उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। वह अलग भी रहने लगता है और स्तन के स्थान पर शीशी से ही बहल जाता है। मनुष्य की विशेषतायें ही किसी के लिए स्नेह, सौजन्य अथवा प्रेम आदि की सुखदायक स्थितियां उत्पन्न करती हैं।
किन्तु मनुष्य की इस विशेषता का स्रोत क्या है। इसका स्रोत भी आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। बताया जा चुका है कि आत्मा से असम्बन्धित मनुष्य शव से अधिक कुछ नहीं होता। जो शव है, मुर्दा है अथवा अचेतन या जड़ है, उनमें किसी प्रकार की प्रेमोत्पादक विशेषता के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य के मन प्राण और शरीर तीनों का संचालन, नियन्त्रण तथा पोषण आत्मा की सूक्ष्म सत्ता द्वारा ही होता है। आत्मा और इन तीनों के बीच जरा-सा व्यवधान आते ही सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सुन्दर, सुगठित और स्वस्थ शरीर की दुर्दशा हो जाती है। प्राणों का स्पन्दन तिरोहित होने लगता है और मन मतवाला होकर मनुष्य को उन्मत्त और पागल बना देता है। ऐसी भयावह स्थिति में संसार का कोई व्यक्ति, कोई आत्मीय और कोई स्वजन सम्बन्धी न तो प्रेम कर सकता है और न स्नेह सौजन्य के सुखद भाव ही प्रदान कर सकता है। यह केवल मनुष्य की अपनी आत्मा ही है, जो उसका सच्चा मित्र, सगा-सम्बन्धी और वास्तविक शक्ति है। इसी के कारण मनुष्य गुणों और विशेषताओं का स्वामी बनकर अपना मूल्य बढ़ाता और पाता है। जीवन में सुख, सौख्य के उत्पादन, अभिवृद्धि और रक्षा के लिये मनुष्य को चाहिये कि वह आत्मा की ही शरण रहे। उसे ही अपना माने, उससे ही प्रेम करे और उसे ही खोजने पाने में अपने जीवन की सार्थकता समझे।
सुख का निवास किसी व्यक्ति, विषय अथवा पदार्थ में नहीं है। उसका निवास आत्मा में ही है। संसार के सारे पदार्थ जड़ और प्रभाव-हीन है। किसी को सुख-दुख देने की उनमें अपनी क्षमता नहीं होती। पदार्थों अथवा विषयों में सुख-दुख का आभास उनके प्रति आत्म-भाव के कारण ही होता है। आत्म-भाव समाप्त हो जाने पर वह अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। हमारी आत्मा ही विभिन्न पदार्थों पर अपना प्रभाव डाल कर उन्हें आकर्षक तथा सुखद बनाती है। अन्यथा संसार के सारे विषय, सारी वस्तुयें, सारे पदार्थ और सारे भोग नीरस, निःसार तथा निरुपयोगी हैं। जड़ होने से सभी कुछ कुरूप तथा अग्राह्य है।
जिस पदार्थ के साथ जितने अंशों में अपनी आत्मा घुली-मिली रहती है, उतने ही अंशों में वह पदार्थ प्रिय, सुखदायी और ग्रहणीय बना रहता है और आत्मा का सम्बन्ध जिस पदार्थ से जितना कम होता जाता है, वह उतना ही अपने लिये कुरूप और अप्रिय बनता जाता है। आनन्द और प्रियता का सम्बन्ध पदार्थों से नहीं स्वयं आत्मा से ही होता है। अस्तु, आत्मा को ही प्यार करना चाहिये, उसे ही तेजस्वी और प्रभावशील बनाना चाहिये, जिससे हमारा सम्बन्ध उसी से दृढ़ हो और उसके उपलक्ष से ही संसार में प्रेम और सुख दे सकें। हमारी अपनी आत्मा ही ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र है। सुख-शांति का मूल आधार है। उन्नति और समृद्धि का बीज उसी में छिपा है, स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्पवृक्ष बाहर नहीं अपनी आत्मा में ही अवस्थित है, आत्मा में ही सब कुछ है और आत्मा स्वयं ही सब कुछ है। उसे ही सर्वस्व और सारे सुखों का मूल और शांति का स्रोत मान कर उसकी उपासना करनी चाहिये। जिसने आत्मा को अपना बना लिया, उसने मानों संसार को अपना बना लिया। जिसने आत्मा को देख लिया, उसने सब कुछ देख लिया और जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसने निश्चय ही सारे सुख, सारे सौख्य और सारे रस, आनन्द एक साथ एक स्थान पर सदा के लिये पा लिये। आत्मा में केन्द्रित प्रियता को वस्तुओं में खोजना अबुद्धिमत्ता ही है। जड़ पदार्थों में न कुछ सुखद है और न दुखद। इस तथ्य की थोड़ी-सी खोज-बीन करने पर सहज ही जाना जा सकता है और सुख के लिए—प्रिय पात्रता के लिए कस्तूरी मृग की तरह बाहर मारे-मारे फिरने की अपेक्षा अन्तर्मुखी हुआ जा सकता है। तिनके के पीछे ताड़ छिपा होने के इसी आश्चर्य को माया कहा जाता है। माया और कुछ नहीं केवल वह अज्ञान है जो बाहरी-मोटी-सामने की-तात्कालिक बातों को ही देखता है और कुछ गहराई में उतर का वस्तुस्थिति समझने का कष्ट उठाने के लिए तत्पर नहीं होता।
तत्वदर्शी ऋषियों ने अनन्त सुख-शान्ति की ओर अंगुलि निर्देश करते हुए कहा है—अन्वेषक प्रकाश को भीतर की ओर मोड़ दो।’ कालाईइल प्रभृति पाश्चात्य दार्शनिक भी यही कहते रहे हैं—‘टर्न द सर्च लाइट इन वार्डस्’।
वस्तुओं और व्यक्तियों में कोई आकर्षण नहीं है। अपनी आत्मीयता जिस किसी से भी जुड़ जाती है वही प्रिय लगने लगता है यह तथ्य कितनी स्पष्ट किन्तु कितना गुप्त है, लोग अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु को रुचिर मधुर मानते हैं और उसे पाने, लिपटाने के लिए आकुल-व्याकुल रहते हैं। प्राप्त होने पर वह आकुलता जैसे ही घटती है वैसे ही वह आकर्षण तिरोहित हो जाता है। किसी कारण यदि ममत्व हट या घट जाय तो वही वस्तु जो कल तक अत्यधिक प्रिय प्रतीत होती थी और जिसके बिना सब कुछ नीरस लगता था। बेकार और निकम्मी लगने लगेगी। वस्तु या व्यक्ति वही—किन्तु प्रियता में आश्चर्यजनक परिवर्तन बहुधा होता रहता है। इसका कारण एक मात्र यही है कि उधर से ममता का आकर्षण कम हो गया।
यह तथ्य यदि समझ लिया जाय तो ममता का आरोपण करके किसी भी वस्तु या व्यक्ति को कितने ही समय तक प्रिय पात्र बनाये रखा जा सकता है। यदि यह आरोपण क्षेत्र बड़ा बनाते चलें तो अपने प्रिय पात्रों की मात्रा एवं संख्या आश्चर्यजनक रीति से बढ़ती चली जायगी और जिधर भी दृष्टि डाली जाय उधर ही रुचिर मधुर बिखरा पड़ा दिखाई देगा और जीवन क्रम में आशाजनक आनन्द, उल्लास भर जायेगा। आत्मविद्या के इस रहस्य को जानकर भी लोक अनजान बने रहते हैं। आनन्द की खोज में—प्रिय पात्रों के पीछे मारे-मारे फिरते हैं। यदि इस माया मरीचिका को छोड़ दिया जाय, जिसे प्रिय पात्र बनाना हो उसी पर ममता बखेर दी जाय तो केवल वही व्यक्ति प्रियपात्र रह जायेंगे जिनकी घनिष्ठता, समीपता, मित्रता, वस्तुतः हितकर है।
बिछुड़ने, एवं खोने पर प्रायः दुख होता है। यदि समझ लिया जाय कि मिलन की तरह वियोग—जन्म की तरह मृत्यु भी अवश्यंभावी है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहा जा सकता है। सांस लेते समय भी यह विदित रहता है कि उसे कुछ ही क्षण पश्चात् छोड़ना पड़ेगा इसलिए श्वास-प्रश्वास की दोनों क्रियाएं समान प्रतीत होती हैं। न एक में दुख होता न दूसरी में सुख। एक का मरण दूसरे का जन्म है। मृत्यु के रुदन के साथ ही किसी घर का जन्मोत्सव बंधा हुआ है। व्यापार में एक को नफा तब होता है जब दूसरे को घाटा पड़ता है। धूप-छांह की तरह—दिन-रात की तरह—सर्दी-गर्मी की तरह यदि मिलन विछोह और हानि-लाभ कोपरस्पर एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से मानकर चला जाय तो राग-द्वेष एवं हानि लाभ के सामान्य सृष्टि क्रम में न कुछ प्रिय लगे न अप्रिय। हमारा अज्ञान ही है जो अकारण हर्षोन्मत्त एवं शोक संतप्त आवेश के ज्वार भाटे में उछलता भटकता रहता है। यदि मायाबद्ध अशुभ चिन्तन से छुटकारा मिल जाय और सृष्टि के अनवरत जन्म, वृद्धि, विनाश के अनिवार्य क्रम को समझ लिया जाय तो मनुष्य शान्त, सन्तुलित, स्थिर, सन्तुष्ट एवं सुखी रह सकता है। ऐसी देवोपम मनोभूमि पल-पल में स्वर्गीय जीवन की सुखद संवेदनाएं सम्मुख प्रस्तुत किये रह सकता है। चिन्तन में समाया हुआ माया विकार ही है जो समुद्र तट पर बैठे अज्ञानी बालक के, ज्वार से प्रसन्न और भाटा से अप्रसन्न होने की तरह हमें उद्विग्न बनाये रहता है।
मल-मूत्र की गठरी के ऊपर प्रकृति ने एक आकर्षक खोल चढ़ाया हुआ है ताकि वह घृणित पिटारा सर्वत्र दुर्गन्ध बखेरता न फिरे। लोग इस आवरण पर मुग्ध हो जाते हैं, रूप, यौवन पर लट्टू होते हैं। सौन्दर्य की शाश्वत प्यास सुकोमल पुष्प से लेकर बाल सुलभ भोलेपन तक से सर्वत्र सहज ही तृप्ति की जा सकती पर विकारी दृष्टि के साथ जुड़ी हुई कामुक लिप्सा नर-नारियों को बेतरह उद्विग्न करती रहती है और उन्हें न चलने योग्य मार्ग पर चलाती है। मूत्र त्याग के घृणित अंगों की तनिक सी खुजली न जाने किससे क्या-क्या नहीं कर लेती। यदि मोहान्ध दृष्टि का पर्दा उठ सका होता तो शारीरिक रूप, यौवन की—यौन लिप्सा की मदोन्मत्ता का नशा सहज ही उतर जाता और पंचभूतों से बने जड़-कलेवर के पीछे आत्मा की ज्योति जगमगाती दीखती। कामुकता का स्थान पवित्र प्रेम भावनाओं ने ग्रहण कर लिया होता और नर-नारी के बीच के सम्बन्ध प्रकृति और पुरुष की तरह एक दूसरे के पूरक बनकर श्रेय साधन में संलग्न रहे होते। आज का नारकीय दाम्पत्य-जीवन तब स्वर्गीय सुषमा बखेर रहा होता। ऐसे उच्च आदर्शों को आधार मानकर बनाये गये गृहस्थ तब स्वर्ग की प्रतिमूर्ति बनकर धरती को आनन्द, उल्लास से भर रहे होते और नर-रत्नों की पीढ़ियां सृजी जातीं। यह पिशाचिनी माया ही है जिसने रूप, सौन्दर्य को परखने का दृष्टि दोष उत्पन्न करके आत्मतत्व को तिरस्कृत और चमड़ी की चमक को गौरव प्रदान किया है।
अपना स्वरूप, अपना लक्ष्य, अपना कर्त्तव्य यदि मनुष्य समय सका होता तो उसका चिन्तन और कर्तृत्व अत्यन्त उच्चकोटि का होता ऐसे नर को नारायण कहा जाता और उसके चरण जहां भी पड़ते वहां धरती धन्य हो जाती। पर अज्ञान के आवरण को क्या कहा जाय जिसने हमें नर-पशु के स्तर पर देखने और उसी प्रकार की रीति-नीति अपनाने के लिए निकृष्टता के गर्त में धकेल दिया है। माया का यही आवरण हमें नारकीय यातनाएं सहन करते हुए रोता, कलपता जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करता है। संसार को जैसा कि हम देखते, समझते हैं वह पूर्व प्रचलित भ्रान्त धारणाओं पर और मस्तिष्क सहित इन्द्रियों के ज्ञान पर आधारित है। यदि हम एक बार इन दोनों आधारों की अप्रामाणिकता और अक्षमता को स्वीकार करलें तथा नये सिरे से अपने सम्बन्ध में, सम्बन्धित व्यक्तियों तथा पदार्थों के सम्बन्ध में समस्त विश्व ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में नये तर्क पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना आरंभ करें तो तथ्य बिलकुल दूसरे ही स्तर के सामने आवेंगे और वही प्रतिपादन सोलहों आने सत्य सिद्ध होगा जिसे वेदान्त दर्शन में निर्धारित किया गया है।
जिस प्रकार हर प्रभात को हम जगते हैं और हर रात को गहरी नींद में सोते हैं ठीक उसी प्रकार थोड़ी अधिक विस्तृत भूमिका में जनम और मरण की प्रक्रिया चलती रहती हैं। सूर्य हर दिन डूबता, उगता है। जीवन भी नियत अवधि में उत्पन्न और समाप्त होता रहता है। जिस तरह एक के बाद दूसरे दिन का लम्बा जीवनयापन चलता रहता है उसी प्रकार एक जन्म के बाद दूसरे जन्म की श्रृंखला चलती है। इसमें न कोई दुख की बात है न शोक की, न डर की। यह तथ्य यदि सामने प्रस्तुत रहे तो फिर जीवन की लम्बी श्रृंखला की योजना इस ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिये। यदि भावी जीवन को उज्ज्वल बनाने की सम्भावना सामने हो तो इसके लिये एक दिन के कष्ट, कठिनाई से व्यतीत करने की बात किसी को अखरती नहीं। ऐसी भूल भी कोई समझदार आदमी नहीं कर सकता कि एक दिन शौक-मौज मनाने के लिये कोई ऐसा अवांछनीय कार्य कर डाला जाय, जिसके लिए जीवन के शेष समस्त दिन विपत्ति में फंसकर व्यतीत करने पड़ें। मनुष्य-जीवन की भोजन व्यवस्था बनाते समय भी यदि यही रीति-नीति अपनाई जा सके तो समझना चाहिये कि अनन्त जीवनों की जुड़ी हुई श्रृंखला का स्वरूप समझ लिया गया। ऐसी दशा में न वस्तुओं से लोभ हो सकता है और न व्यक्तियों से मोह। तब केवल वस्तुओं के सदुपयोग और व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यपालन का भाव ही मन में उठता रह सकता है।
एक जन्म को ही पूरा जीवन मान बैठने से मनुष्य आज ही जी भरकर शौक-मौज करने के लिये आतुर होता है और भविष्य को अन्धकारमय बनाता है। यदि अनन्त जीवन में एक-एक जन्म को एक दिन की तरह नगण्य महत्व का माना जाय तो फिर विद्यार्थी के विद्याध्ययन, पहलवान और कृषक की तरह अनवरत कष्ट साधन करने के लिए उत्साह बना रहेगा और उज्ज्वल भविष्य की आस में आज की कठिनाइयों को तुच्छ माना जायेगा। पर होता ऐसा कहां है? इसका कारण वर्तमान को ही सब कुछ मान बैठने का मायावादी अज्ञान ही है। इसी में फंसकर मनुष्य दुर्बुद्धि अपनाता और पापकर्म करता है यदि माया का पर्दा हट जाय तो फिर बाल-क्रीड़ाओं को छोड़ कर वयस्कों और बुद्धिमानों जैसी गति-विधियां अपनाने की ही प्रवृत्ति बनेगी।
हम सब सराय में ठहरे हुये मुसाफिरों की तरह ही दिन व्यतीत कर रहे हैं। जल प्रवाह में बहते हुये तिनकों की तरह ही इकट्ठे हो गये हैं। जब मिल ही गये तो सराय के नियमों का सड़क पर चलने के कानूनों का क्षेत्र के नागरिक कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा, इस दृष्टि के विकसित होने पर यह अज्ञान हट जाता है कि कोई हमारा है या हम किसी के हैं। सब ईश्वर के हैं—और ईश्वर ही सबका हितू है। प्रत्येक प्राणी अपनी कर्म रज्जु में बंधा अपनी धुरी पर घूम रहा है। समय का परिपाक बहुतों को परस्पर जुड़ता और बिछुड़ता रहता है। यह सत्य यदि समझ में आ जाय तो न किसी के मोह बन्धन में बंधा जाय, न बांधा जाय। आत्मीयता के विस्तार द्वारा सम्पन्न होने वाला प्रेम हर किसी पर परिपूर्ण मात्रा में बखेरा जाय, पर उसमें विवेक का समुचित पुट रहे। परिवारी लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, पक्षपात और मोह के कारण उन्हें अनुचित लाभ देने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उससे हर किसी का घोर अहित होता है। मुफ्त में अनावश्यक सहायता पाकर परिवार के लोग मुफ्तखोर बनते हैं और अपने श्रम-साधनों से जो लोक-मंगल सम्भव था उससे समाज को वंचित रहना पड़ता है और व्यक्ति परमार्थ का कल्याणकारी लाभ लेने से वंचित रह जाता है। यह माया बन्धनों का परिणाम ही है जिसने मोह जाल में जकड़ कर विश्व हित को श्रेय साधना से वंचित करके पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने में भारी व्यवधान प्रस्तुत किया।
वस्तुएं हमें इसलिये मिलती हैं कि उनका श्रेष्ठतम सदुपयोग करके उनसे स्व-पर कल्याण की व्यवस्था बनाई जाय। साधन जड़ जगत के अंग हैं और वे रंग रूप बदलते हुए इस जगत की शोभा बढ़ाते रहने के लिए हैं। उन्हें अपने गर्व-गौरव का, विलास वैभव का आधार बनाकर संग्रह करते चलें। अहंकार का पोषण, तृष्णा की तुष्टि अथवा विलासिता के अभिवर्धन में धन को—शारीरिक, मानसिक विभूतियों को नियोजित रखा जाय तो उत्कृष्ट जीवन जी सकने का द्वार अवरुद्ध ही बना रहेगा। संकीर्ण और स्वार्थी जिन्दगी ही जियी जा सकेगी और इस कुचक्र में यह सुर-दुर्लभ अक्सर निरर्थक ही चला जायेगा।
शरीर और मन को अपना आपा मान बैठना और उसकी वासनाओं, तृष्णाओं की पूर्ति में इतना निमग्न हो जाना कि आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य पूरी तरह विस्मृत हो जाय, ये दूरदर्शितापूर्ण नहीं है। शारीरिक और मानसिक उपलब्धियों के लिये जितना श्रम किया जाता है और मनोयोग लगाया जाता है, जोखिम उठाया जाता है उतना ही विनियोग यदि आत्मोत्कर्ष के लिये—आत्मबल सम्पादन के लिये लगाया जा सके तो मनुष्य इसी जीवन में महामानव बन सकता है और उन विभूतियों को करतलगत कर सकता है जो देवदूतों में पाई जाती हैं। इतना उच्चकोटि का लाभ छोड़कर नगण्य-सी लिप्साओं में डूबे हुये न करने योग्य काम करना—उनके कटु-कर्म—परिपाक सहना, किसी विवेकवान के लिए उपयुक्त न होगा। किन्तु देखा जाता है कि अधिकांश व्यक्ति उचित छोड़कर अनुचित का, लाभ छोड़कर हानि का रास्ता अपनाते हैं इसे क्या कहा जाय? यह माया का खेल ही है। जिससे भ्रमित होकर मनुष्य जल में थल-थल में जल देखने की तरह हानि को लाभ और लाभ को हानि समझता है। अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारता है। माया विमुग्ध होकर ही मनुष्य अपने उच्च स्तर से अपनी दुर्बलताओं के कारण अधः पतित होता है और दुःख क्लेश भरा नरक भोगता है अन्यथा मनुष्य को इस विश्व के साथ सम्पर्क बनाकर सुखानुभूति प्राप्त कराने वाले जो तीन उपकरण मिले हैं यदि उनका ठीक तरह उपयोग किया जा सके तो जीवन अति सुन्दर और मधुर बन सकता है। इन तीन उपकरणों के नाम हैं। (1) अन्तरात्मा (2) मन (3) इन्द्रिय समूह।
इन्द्रियों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रिया में ही उन्हें पग-पग पर असाधारण सरसता अनुभव होती है। पेट भरने के लिए भोजन करना स्वाभाविक है। भगवान की कैसी महिमा है कि उसने दैनिक जीवन की शरीर यात्रा भर की नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया को कितना सरस बना दिया है। उपयुक्त भोजन करते हुये जीव को कितना रस मिलता है और चित्त को उस अनुभूति से कैसे प्रसन्नता होती है।
आंख का साधारण काम है वस्तुओं को देखना ताकि हमारी जीवन यात्रा ठीक तरह चलती रह सके। पर आंखों में कितनी अद्भुत विशेषता भर दी है कि वह रूप, सौन्दर्य, कौतुक, कौतूहल जैसी रस भरी अनुभूतियां ग्रहण करके चित्त को प्रफुल्लित बनाती हैं। संसार में उत्पादन, परिपुष्टि, विनाश का क्रम नितान्त स्वाभाविक है। मध्यवर्ती स्थिति में हर चीज तरुण होती है और सुन्दर लगती है। क्या पुष्प क्या मनुष्य हर किसी को तीनों स्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। मध्यकाल सौन्दर्य लगता है। वस्तुतः यह तीनों ही स्थितियां अपने क्रम, अपने स्थान और अपने समय पर सुन्दर हैं। पर आंखों को सुन्दर-असुन्दर का भेद करके मध्य स्थिति को सुन्दर समझने की कुछ अद्भुत विशेषता मिली है। फलस्वरूप जो कुछ उभरता हुआ विकसित, परिपुष्ट दीखता है सो सुन्दर लगता है। सुन्दर असुन्दर का तात्विक दृष्टि से यहां कुछ भी अस्तित्व नहीं है। पर हमारी अद्भुत आंखें ही हैं जो अपनी सौन्दर्यानुभूति वाली विशेषता के कारण हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्धित समीपवर्ती वस्तुओं में से सौन्दर्य वाला भाग देखतीं, आनन्द अनुभव करतीं, उल्लसित और पुलकित होती हैं। चित्त को प्रसन्न करती हैं।
इसी प्रकार जननेन्द्रिय की प्रक्रिया है। प्रजनन मक्खी मच्छरों, कीट-पतंगों, बीज अंकुरों में भी चलता रहता है। यह सृष्टि का सरल स्वाभाविक क्रम है पर हमारी जननेन्द्रिय में कैसा अजीब उल्लास सराबोर कर दिया है कि संभोग के क्षण ही नहीं—उसकी कल्पना भी मन के कोने-कोने में सिहरन पुलकन, उमंग और आतुरता भर देती है। तत्वतः बात कुछ भी नहीं है। दो शरीरों के दो अवयवों का स्पर्श—इसमें क्या अनोखापन है? क्या अद्भुतता है? क्या उपलब्धि है? फिर स्पर्श का कुछ प्रभाव हो भी तो उसकी कल्पना से किस प्रकार, क्यों, किस लिये चित्त को बेचैन करने वाली ललक पैदा होनी चाहिये? बात कुछ भी नहीं है। मात्र जननेन्द्रिय की बनावट में एक अद्भुत प्रकार की सरसता का समावेश मात्र है जो हमें सामान्य स्वाभाविक दाम्पत्य-जीवन के वास्तविक या काल्पनिक प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र में एक विचित्र प्रकार की रसानुभूति उत्पन्न करके—जीने भर के लिये प्रयुक्त हो सकने वाले जीवन को निरन्तर उमंगों से भरता रहता है।
ऊपर जीभ, आंख और जननेन्द्रिय की चर्चा हुई, कान और नाक के बारे में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। यहां पान भाग वाला इन्द्रिय समूह अपने साथ रसानुभूति की विलक्षणता इसलिये धारण किये हुये हैं कि सरस, स्वाभाविक सामान्य जीवन क्रम ऐसे ही नीरस ढर्रे का जीने भर के लिये मिला हुआ प्रतीत न हो वरन् उसमें हर घड़ी उत्साह, उल्लास, रस, आनन्द बना रहे और उसे उपलब्ध करते रहने के लिये जीवन की उपयोगिता, सार्थकता और सरसता का भान होता रहे। इन्द्रिय समूह हमें इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध है। यदि उनका उचित, संयमित, विवेकपूर्ण, व्यवस्था पूर्वक उपयोग किया जा सके, तो हमारा भौतिक सांसारिक जीवन पग-पग पर सरसता, आनन्द उपलब्ध करता रह सकता है।
दूसरा उपकरण मन इसलिए मिला है कि संसार में जो कुछ चेतन है उसके साथ अपनी चेतना का स्पर्श करके और भी ऊंचे स्तर की आनन्दानुभूति प्राप्त करे। इन्द्रियां जड़ शरीर से सम्बन्धित हैं। जड़ पदार्थों को स्पर्श करके—उस संसर्ग का सुख लूटती हैं। जड़ का जड़ से स्पर्श भी कितना सुखद हो सकता है, इस विचित्रता का अनुभव हमें इन्द्रियों के माध्यम से होता है। चेतन का चेतन के साथ, जीवधारी का जीवधारी के साथ स्पर्श—सम्पर्क होने से मित्रता, ममता, मोह, स्नेह, सद्भाव, घनिष्ठता, दया, करुणा, मुदिता जैसी अनुभूतियां होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष, घृणा जैसे भाव भी उत्पन्न होते हैं पर उनका अस्तित्व है इसीलिए कि मित्रता के वातावरण में सम्पर्क, संसर्ग का आनन्द बिखरता रहे, यदि अन्धकार न हो तो प्रकाश की विशेषता ही नष्ट हो जाय। वस्तुतः मन की बनावट दूसरों के सम्पर्क, सहयोग, स्नेह भावों के आदान-प्रदान का सुख प्राप्त करने में है। मेले-ठेलों में सभा सम्मेलनों में जाने की इच्छा इसीलिए उठती है उन जन संकुल स्थानों में व्यक्तियों की घनिष्ठता न सही समीपता का अदृश्य सुख तो अनायास मिलता ही है।
चूंकि इन्द्रिय सुख और जन सम्पर्क की घनिष्ठता में सहायक एक और नया माध्यम सभ्यता के विकास के साथ-साथ बनकर खड़ा हो गया है इसलिये अब प्रिय वह भी लगने लगा है—इस तीसरे मनुष्य कृत—आकर्षण तत्व का नाम है—धन में स्वभावतः कोई आकर्षण नहीं। इसमें इन्द्रिय समूह या मन को पुलकित करने वाली कोई सीधी क्षमता नहीं है। धातु के सिक्के या कागज के टुकड़े भला आदमी के लिए प्रत्यक्षतः क्यों आकर्षक हो सकते हैं। पर चूंकि वर्तमान समाज व्यवस्था के अनुसार धन के द्वारा इन्द्रिय सुख के साधन प्राप्त होते हैं। मैत्री भी सम्भव होती है। इसलिए धन भी प्रकारान्तर रूप से मन का प्रिय विषय बन गया। अस्तु धन की गणना भी सुखदायक माध्यमों से जोड़ ली गई है।
तीन शरीरों को जीवात्मा धारण किये हुए है। तीनों की तीन रसानुभूतियां हैं। ऊपर दो की चर्चा हो चुकी। स्थूल शरीर की सरसता-इन्द्रिय समूह के साथ जुड़ी हुई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे सुख इन्द्रियों द्वारा ही मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है। मन की सरसता मैत्री पर, जन सम्पर्क पर अवलम्बित है। परिवार मोह से लेकर समाज सम्बन्ध, नेतृत्व, सम्मिलन, उत्सव, आयोजन जैसे सम्पर्क परक अवसर मन को सुख देते हैं। घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने की सूक्ष्म सम्वेदना उत्पन्न करके वह समाज की अनेक हलचलों से भी अपने को बांध लेता है और उन घटना क्रमों में खट्टी-मीठी अनुभूतियां उपलब्ध करता है। उपन्यास, सिनेमा, अखबार रेडियो आदि मन को इसी आधार पर आकर्षित करते और प्रिय लगते हैं।
तीसरा रसानुभूति उपकरण है—अन्तरात्मा उसका कार्य क्षेत्र ‘कारण शरीर’ है। उसमें उत्कृष्टता, उत्कर्ष, प्रगति, गौरव की प्रवृत्ति रहती है जो उच्च भावनाओं के माध्यम से चरितार्थ होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता और सन्मार्गगामिता प्रखर होती रहे इसके लिए उसमें भी एक रसानुभूति विद्यमान है—उसका नाम है वर्चस्व, यश कामना, नेतृत्व, गौरव प्रदर्शन। उस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अगणित प्रकार की सफलतायें प्राप्त करता है ताकि वह स्वयं दूसरों की तुलना में अपने आपको श्रेष्ठ, पुरुषार्थी, पराक्रमी, बुद्धिमान अनुभव करके सुख प्राप्त करे और दूसरे लोग भी उसकी विशेषताओं, विभूतियों से प्रभावित होकर उसे यश, मान प्रदान करें।
संक्षेप में यह मनुष्य के तीन शरीरों की—तीन रसानुभूतियों की चर्चा हुई। हमारी अगणित योजनायें—इच्छा, आकांक्षायें गतिविधियां इन्हीं तीन मल प्रवृत्तियों के इर्द−गिर्द घूमती हैं। जो कुछ मनुष्य सोचता और करता है उसे तीन भोगों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान ने यह तीन उपहार जीवन को सरसता से भरा पूरा रखने के लिये दिये हैं। साथ ही उनका अस्तित्व इसलिये भी है कि व्यक्ति निरन्तर सक्रिय बना रहे। इन सुखानुभूतियों को प्राप्त करने के लिये उसके तीनों शरीर निरन्तर जुटे रहें। आलस्य, अवसाद की उदासीनता, नीरसता की स्थिति सामने आकर खड़ी न हो जाय और जीवन को आनन्द रहित भार रूप न बना दे। सक्रियता के आधार पर चल रहे सृष्टि क्रम को अवरुद्ध न करदे। अन्तरात्मा, मन और इन्द्रिय समूह को यदि सही मार्ग पर चलने का अवसर मिलता रहे तो जीवन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो सकता है। भूल मनुष्य की तब आरम्भ होती है जब वह इन तीनों रसानुभूतियों को अमर्यादित होकर—अनावश्यक मात्रा में—अति शीघ्र, बिना उचित मूल्य चुकाये प्राप्त करने के लिये आकुल, आतुर हो उठता है और लूट-खसोट की मनोवृत्ति अपनाकर अवांछनीय गतिविधियां अपना लेता है। विग्रह इसी से उत्पन्न होता है। पाप का कारण यही उतावली है। जीवन में अव्यवस्था और अस्त-व्यस्तता इसी से उत्पन्न होती। पतन इसी भूल का परिणाम है अपराधी, दुष्ट और घृणित बनने का कारण उन उपलब्धियों के लिये अनुचित मार्ग को अपनाना ही है। उतावला व्यक्ति आतुरता में विवेक खो बैठता है और औचित्य को भूलकर बहुत जल्दी—अधिक मात्रा में उपरोक्त सुखों को पाने के लिए असन्तुष्ट होकर एक प्रकार से उच्छृंखल हो उठता है। यह अमर्यादित स्थिति उसके लिए विपत्ति बनकर सामने आती है। सरल स्वाभाविक रीति से जो शान्ति पूर्वक मिल रहा था—मिलता रह सकता था—वह भी हाथ से चला जाता है और शारीरिक रोग, मानसिक उद्वेग—सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक अभाव आत्मिक अशान्ति के संकटों से घिरा हुआ जीवन नरक बन जाता है। अधिक के लिये उतावला मनुष्य सरसता स्वाभाविकता को भी खोकर उलटा शोक-संताप, कष्ट-क्लेश एवं अभाव, दारिद्र्य में फंस जाता है। आमतौर से मनुष्य यह भूल करते हैं। इसी भूल को माया, अज्ञान, अविद्या नामों से पुकारते हैं। यह भूल ही ईश्वर प्रदत्त पग-पग पर मिलती रहने वाली सरसता से वंचित करती है और इसी के कारण जीव ऊंचा उठने के स्थान पर नीचे गिरता है।
अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मनुष्य के चिन्तन और कर्तव्य को अमर्यादित न होने देने—अवांछनीयता न अपनाने के लिए आवश्यक विवेक और साहस उत्पन्न करता है मनुष्य अपने अस्तित्व को, लक्ष्य को व्यवहार को सही तरह समझे। सही मार्ग को अपनाकर सही परिणाम उपलब्ध करते हुए, प्रगति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ता चले। अपूर्णता से पूर्णता में विकसित हो। यही मार्गदर्शक करता—इसका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना आत्मविद्या का मूल प्रयोजन है।
यह स्मरण रखा जाना चाहिए मानव का निर्माण जड़ एवं चेतन दोनों के युग्म से हुआ है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक हमारी सभी इन्द्रियां क्रियाशील हैं और शरीर में हलचल है, लेकिन जिस क्षण चेतना या आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर मिट्टी का ढेला मात्र ही रहता है। कोई स्पन्दन, कोई क्रिया, कोई सार्थकता नहीं रह पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर एवं आत्मा का संयोग जहां जीवात्मा में विराट् शक्ति का स्रोत है वहां आत्मा से रहित शरीर का कोई मूल्य नहीं। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण हम अपने शरीर के सुख साधन जुटाने में खर्च करते हैं और इन्द्रियजन्य भोगों में मरते-खपते रहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय तक भी हम अपनी वासनाओं, तृष्णाओं एवं लिप्साओं को तुष्ट नहीं कर पाते।
जीवन के समग्र उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि हम शरीर एवं आत्मा दोनों के समन्वित विकास, परिष्कार एवं तुष्टि-पुष्टि का दृष्टिकोण बनावें। एक को ही सिर्फ विकसित करें और एक को उपेक्षित करें—ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता।
वास्तविक बात यह है कि संसार के सारे पदार्थ जड़ होते हैं। जड़ तो जड़ ही है। उसमें अपनी कोई क्षमता नहीं होती। न तो जड़ पदार्थ किसी को स्वयं सुख दें सकते हैं और न दुःख। क्योंकि उनमें न तो सुखद तत्व होते हैं और न दुःखद तत्व और न उनमें सक्रियता ही होती है, जिससे वे किसी को अपनी विशेषता से प्रभावित कर सकें। यह मनुष्य का अपना आत्म-तत्व ही होता है, जो उससे सम्बन्ध स्थापित करके उसे सुखद या दुःखद बना लेता है। आत्म तत्व की उन्मुखता ही किसी पदार्थ को किसी के लिये सुखद और किसी के लिये दुःखद बना देती है।
जिस समय मनुष्य का आत्म-तत्व सुखोन्मुख होकर पदार्थ से सम्बन्ध स्थापित करता है, वह सुखद बन जाता है और जब आत्मतत्व दुःखोन्मुख होकर सम्बन्ध स्थापित करता है, तब वही पदार्थ उसके लिये दुःखद बन जाता है। संसार के सारे पदार्थ जड़ हैं, वे अपनी ओर से न तो किसी को सुख दें सकते हैं और दुःख। यह मनुष्य का अपना आत्म-तत्व ही होता है, जो सम्बन्धित होकर उनको दुःखदायी अथवा सुखदायी बना देता है। यह धारणा कि सुख की उपलब्धि पदार्थों द्वारा होती है, सर्वथा मिथ्या और अज्ञानपूर्ण है।
किन्तु खेद है कि मनुष्य अज्ञानवश सुख-दुःख के इस रहस्य पर विश्वास नहीं करते और सत्य की खोज संसार के जड़ पदार्थों में किया करते हैं। पदार्थों को सुख का दाता मानकर उन्हें ही संचय करने में अपना बहुमूल्य जीवन बेकार में गंवा देते हैं। केवल इतना ही नहीं कि वे सुख आत्मा में नहीं करते बल्कि पदार्थों के चक्कर में फंसकर उनका संचय करने लिये अकरणीय कार्य तक किया करते हैं। झूंठ, फरेब, मक्कारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के अपराध और पाप तक करने में तत्पर रहते हैं। सुख का निवास पदार्थों में नहीं आत्मा में है। उसे खोजने और पाने के लिये पदार्थों की ओर नहीं आत्मा की ओर उन्मुख होना चाहिए।
पदार्थों का उपभोग इन्द्रियों द्वारा होता है। इन्द्रियों के सक्रिय और सजीव होने से ही किसी रस, सुख अथवा आनन्द की अनुभूति होती है। जब तक मनुष्य सक्षम अथवा युवा बना रहता है, उसकी इन्द्रियां सतेज बनी रहती हैं। पदार्थ और विषयों का आनन्द मिलता रहता है। पर जब मनुष्य वृद्ध अथवा अशक्त हो जाता है—उन्हीं पदार्थों में जिनमें पहले विभोर कर देने वाला आनन्द मिलता था, एकदम नीरस और स्वादहीन लगने लगते हैं। उनका सारा सुख न जाने कहां विलीन हो जाता है। वास्तविक बात यह है कि अशक्तता की दशा अथवा वृद्धावस्था में इन्द्रियां निर्बल तथा अनुभवशीलता से शून्य हो जाती हैं। उनमें किसी पदार्थ का रस लेने की शक्ति नहीं रहती। इन्द्रियों का शैथिल्य ही पदार्थों को नीरस, असुखद तथा निस्सार बना देता है।
वृद्धावस्था ही क्यों? बहुत बार यौवनावस्था में भी सुख की अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। इन्द्रियों में कोई रोग लग जाने अथवा उनको चेतना हीन बना देने वाली कोई घटना घटित हो जाने पर भी उनकी रसानुभूति की शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे रसेन्द्रिय जिह्वा में छाले पड़ जायें तो मनुष्य कितने ही सुस्वाद पदार्थों का सेवन क्यों न करे, उसे उसमें किसी प्रकार का आनन्द न मिलेगा। पाचन क्रिया निर्बल हो जाय तो कोई भी पौष्टिक पदार्थ बेकार हो जायेगा। आंखें विकार युक्त हो जायें तो सुन्दर से सुन्दर दृश्य भी कोई आनन्द नहीं दें पाते। इस प्रकार देख सकते हैं कि सुख पदार्थ में नहीं बल्कि इन्द्रियों की अनुभूति शक्ति में है।
अब देखना यह है कि इन्द्रियों की शक्ति क्या है? बहुत बार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, जिनकी आंखें देखने में सुन्दर स्वच्छ तथा विकार-हीन होती हैं, लेकिन उन्हें दिखलाई नहीं पड़ता। परीक्षा करने पर पता चलता है कि आंखों का यन्त्र भी ठीक है। उनमें आने-जाने वाली नस-नाड़ियों की व्यवस्था भी ठीक है। तथापि दिखलाई नहीं देता। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियां हाथ-पांव, नाक-कान आदि की भी दशा हो जाती है। सब तरफ से सब वस्तुयें ठीक होने पर भी इन्द्रिय निष्क्रिय अथवा निरनुभूति ही रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि रस की अनुभूति इन्द्रियों की स्थूल बनावट से नहीं होती। बल्कि इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है, जो रस की अनुभूति कराती है। वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है चेतना, जो सारे शरीर और मन प्राण में ओत-प्रोत रहकर मनुष्य की इन्द्रियों को रसानुभूति की शक्ति प्रदान करती है। इसी सब ओर से शरीर में ओत-प्रोत चेतना को आत्मा कहते हैं। आनन्द अथवा सुख का निवास आत्मा में ही है। उसी की शक्ति से उसकी अनुभूति होती है और वही जीव रूप में उसका अनुभव भी करती है। सुख न पदार्थों में है और न किसी अन्य वस्तु में। वह आत्मा में ही जीवात्मा द्वारा अनुभव किया जाता है।
मनुष्य की अपनी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा से रहित वह एक मिट्टी का पिण्ड मात्र ही है। शरीर से जब आत्मा का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तो वह मुर्दा हो जाता है। शीघ्र ही उसे बाहर करने और जलाने दफनाने का प्रबन्ध किया जाता है। संसार के सारे सम्बन्ध आत्मा द्वारा ही सम्बन्धित हैं। जब तक जिसमें आत्मभाव बना रहता है, उसमें प्रेम और सुख आदि की अनुभूति बनी रहती है और जब यह आत्मीयता समाप्त हो जाती है वही वस्तु या व्यक्ति अपने लिये कुछ भी नहीं रह जाता। किसी को अपना मित्र बड़ा प्रिय लगता है। उससे मिलने पर हार्दिक आनन्द की उपलब्धि होती है। न मिलने से बेचैनी होती है। किन्तु जब किन्हीं कारणोंवश उससे मैत्री भाव समाप्त हो जाता है अथवा आत्मीयता नहीं रहती तो वह मित्र अपने लिए, एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। उसके मिलने न मिलने में किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं होता। बहुत बार तो उससे इतनी विमुखता हो जाती है कि मिलने अथवा दिखने पर अन्यथा अनुभव होता है। प्रेम, सुख और आनन्द की सारी अनुभूतियां आत्मा से ही सम्बन्धित होती हैं, किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा पदार्थ से नहीं। सुख का संसार आत्मा में ही बसा हुआ है। उसे उसमें खोजना चाहिये। सांसारिक विषयों अथवा वस्तुओं में भटकते रहने से वही दशा और परिणाम सामने आयेगा, जो मरीचिका में भूल मृग के सामने आता है।
मनुष्य की अपनी विशेषता ही उसके लिये उपयोगिता तथा स्नेह सौजन्य उपार्जित करती है। विशेषता समाप्त होते ही मनुष्य का मूल्य भी समाप्त हो जाता है और तब वह न तो किसी के लिये आकर्षक रह जाता है और न प्रिय! इस बात को समझने के लिए सबसे अधिक निकट रहने वाले मां और बच्चे को ले लीजिये। माता से जब तक बच्चा दूध और जीवन रस पाता रहता है, उसके शरीर से अवयव की तरह चिपटा रहता है। उसे मां से असीम प्रेम होता है। जरा देर को भी वह मां से अलग नहीं हो सकता। मां उसे छोड़कर कहीं गई नहीं कि वह रोने लगता है। किन्तु जब इसी बालक को अपनी सुरक्षा तथा जीवन के लिये मां की गोद और दूध की आवश्यकता नहीं रहती अथवा रोग आदि के कारण मां की यह विशेषता समाप्त हो जाती है तो बच्चा उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। वह अलग भी रहने लगता है और स्तन के स्थान पर शीशी से ही बहल जाता है। मनुष्य की विशेषतायें ही किसी के लिए स्नेह, सौजन्य अथवा प्रेम आदि की सुखदायक स्थितियां उत्पन्न करती हैं।
किन्तु मनुष्य की इस विशेषता का स्रोत क्या है। इसका स्रोत भी आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। बताया जा चुका है कि आत्मा से असम्बन्धित मनुष्य शव से अधिक कुछ नहीं होता। जो शव है, मुर्दा है अथवा अचेतन या जड़ है, उनमें किसी प्रकार की प्रेमोत्पादक विशेषता के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य के मन प्राण और शरीर तीनों का संचालन, नियन्त्रण तथा पोषण आत्मा की सूक्ष्म सत्ता द्वारा ही होता है। आत्मा और इन तीनों के बीच जरा-सा व्यवधान आते ही सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सुन्दर, सुगठित और स्वस्थ शरीर की दुर्दशा हो जाती है। प्राणों का स्पन्दन तिरोहित होने लगता है और मन मतवाला होकर मनुष्य को उन्मत्त और पागल बना देता है। ऐसी भयावह स्थिति में संसार का कोई व्यक्ति, कोई आत्मीय और कोई स्वजन सम्बन्धी न तो प्रेम कर सकता है और न स्नेह सौजन्य के सुखद भाव ही प्रदान कर सकता है। यह केवल मनुष्य की अपनी आत्मा ही है, जो उसका सच्चा मित्र, सगा-सम्बन्धी और वास्तविक शक्ति है। इसी के कारण मनुष्य गुणों और विशेषताओं का स्वामी बनकर अपना मूल्य बढ़ाता और पाता है। जीवन में सुख, सौख्य के उत्पादन, अभिवृद्धि और रक्षा के लिये मनुष्य को चाहिये कि वह आत्मा की ही शरण रहे। उसे ही अपना माने, उससे ही प्रेम करे और उसे ही खोजने पाने में अपने जीवन की सार्थकता समझे।
सुख का निवास किसी व्यक्ति, विषय अथवा पदार्थ में नहीं है। उसका निवास आत्मा में ही है। संसार के सारे पदार्थ जड़ और प्रभाव-हीन है। किसी को सुख-दुख देने की उनमें अपनी क्षमता नहीं होती। पदार्थों अथवा विषयों में सुख-दुख का आभास उनके प्रति आत्म-भाव के कारण ही होता है। आत्म-भाव समाप्त हो जाने पर वह अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। हमारी आत्मा ही विभिन्न पदार्थों पर अपना प्रभाव डाल कर उन्हें आकर्षक तथा सुखद बनाती है। अन्यथा संसार के सारे विषय, सारी वस्तुयें, सारे पदार्थ और सारे भोग नीरस, निःसार तथा निरुपयोगी हैं। जड़ होने से सभी कुछ कुरूप तथा अग्राह्य है।
जिस पदार्थ के साथ जितने अंशों में अपनी आत्मा घुली-मिली रहती है, उतने ही अंशों में वह पदार्थ प्रिय, सुखदायी और ग्रहणीय बना रहता है और आत्मा का सम्बन्ध जिस पदार्थ से जितना कम होता जाता है, वह उतना ही अपने लिये कुरूप और अप्रिय बनता जाता है। आनन्द और प्रियता का सम्बन्ध पदार्थों से नहीं स्वयं आत्मा से ही होता है। अस्तु, आत्मा को ही प्यार करना चाहिये, उसे ही तेजस्वी और प्रभावशील बनाना चाहिये, जिससे हमारा सम्बन्ध उसी से दृढ़ हो और उसके उपलक्ष से ही संसार में प्रेम और सुख दे सकें। हमारी अपनी आत्मा ही ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र है। सुख-शांति का मूल आधार है। उन्नति और समृद्धि का बीज उसी में छिपा है, स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्पवृक्ष बाहर नहीं अपनी आत्मा में ही अवस्थित है, आत्मा में ही सब कुछ है और आत्मा स्वयं ही सब कुछ है। उसे ही सर्वस्व और सारे सुखों का मूल और शांति का स्रोत मान कर उसकी उपासना करनी चाहिये। जिसने आत्मा को अपना बना लिया, उसने मानों संसार को अपना बना लिया। जिसने आत्मा को देख लिया, उसने सब कुछ देख लिया और जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसने निश्चय ही सारे सुख, सारे सौख्य और सारे रस, आनन्द एक साथ एक स्थान पर सदा के लिये पा लिये। आत्मा में केन्द्रित प्रियता को वस्तुओं में खोजना अबुद्धिमत्ता ही है। जड़ पदार्थों में न कुछ सुखद है और न दुखद। इस तथ्य की थोड़ी-सी खोज-बीन करने पर सहज ही जाना जा सकता है और सुख के लिए—प्रिय पात्रता के लिए कस्तूरी मृग की तरह बाहर मारे-मारे फिरने की अपेक्षा अन्तर्मुखी हुआ जा सकता है। तिनके के पीछे ताड़ छिपा होने के इसी आश्चर्य को माया कहा जाता है। माया और कुछ नहीं केवल वह अज्ञान है जो बाहरी-मोटी-सामने की-तात्कालिक बातों को ही देखता है और कुछ गहराई में उतर का वस्तुस्थिति समझने का कष्ट उठाने के लिए तत्पर नहीं होता।
तत्वदर्शी ऋषियों ने अनन्त सुख-शान्ति की ओर अंगुलि निर्देश करते हुए कहा है—अन्वेषक प्रकाश को भीतर की ओर मोड़ दो।’ कालाईइल प्रभृति पाश्चात्य दार्शनिक भी यही कहते रहे हैं—‘टर्न द सर्च लाइट इन वार्डस्’।
वस्तुओं और व्यक्तियों में कोई आकर्षण नहीं है। अपनी आत्मीयता जिस किसी से भी जुड़ जाती है वही प्रिय लगने लगता है यह तथ्य कितनी स्पष्ट किन्तु कितना गुप्त है, लोग अमुक व्यक्ति या अमुक वस्तु को रुचिर मधुर मानते हैं और उसे पाने, लिपटाने के लिए आकुल-व्याकुल रहते हैं। प्राप्त होने पर वह आकुलता जैसे ही घटती है वैसे ही वह आकर्षण तिरोहित हो जाता है। किसी कारण यदि ममत्व हट या घट जाय तो वही वस्तु जो कल तक अत्यधिक प्रिय प्रतीत होती थी और जिसके बिना सब कुछ नीरस लगता था। बेकार और निकम्मी लगने लगेगी। वस्तु या व्यक्ति वही—किन्तु प्रियता में आश्चर्यजनक परिवर्तन बहुधा होता रहता है। इसका कारण एक मात्र यही है कि उधर से ममता का आकर्षण कम हो गया।
यह तथ्य यदि समझ लिया जाय तो ममता का आरोपण करके किसी भी वस्तु या व्यक्ति को कितने ही समय तक प्रिय पात्र बनाये रखा जा सकता है। यदि यह आरोपण क्षेत्र बड़ा बनाते चलें तो अपने प्रिय पात्रों की मात्रा एवं संख्या आश्चर्यजनक रीति से बढ़ती चली जायगी और जिधर भी दृष्टि डाली जाय उधर ही रुचिर मधुर बिखरा पड़ा दिखाई देगा और जीवन क्रम में आशाजनक आनन्द, उल्लास भर जायेगा। आत्मविद्या के इस रहस्य को जानकर भी लोक अनजान बने रहते हैं। आनन्द की खोज में—प्रिय पात्रों के पीछे मारे-मारे फिरते हैं। यदि इस माया मरीचिका को छोड़ दिया जाय, जिसे प्रिय पात्र बनाना हो उसी पर ममता बखेर दी जाय तो केवल वही व्यक्ति प्रियपात्र रह जायेंगे जिनकी घनिष्ठता, समीपता, मित्रता, वस्तुतः हितकर है।
बिछुड़ने, एवं खोने पर प्रायः दुख होता है। यदि समझ लिया जाय कि मिलन की तरह वियोग—जन्म की तरह मृत्यु भी अवश्यंभावी है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहा जा सकता है। सांस लेते समय भी यह विदित रहता है कि उसे कुछ ही क्षण पश्चात् छोड़ना पड़ेगा इसलिए श्वास-प्रश्वास की दोनों क्रियाएं समान प्रतीत होती हैं। न एक में दुख होता न दूसरी में सुख। एक का मरण दूसरे का जन्म है। मृत्यु के रुदन के साथ ही किसी घर का जन्मोत्सव बंधा हुआ है। व्यापार में एक को नफा तब होता है जब दूसरे को घाटा पड़ता है। धूप-छांह की तरह—दिन-रात की तरह—सर्दी-गर्मी की तरह यदि मिलन विछोह और हानि-लाभ कोपरस्पर एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से मानकर चला जाय तो राग-द्वेष एवं हानि लाभ के सामान्य सृष्टि क्रम में न कुछ प्रिय लगे न अप्रिय। हमारा अज्ञान ही है जो अकारण हर्षोन्मत्त एवं शोक संतप्त आवेश के ज्वार भाटे में उछलता भटकता रहता है। यदि मायाबद्ध अशुभ चिन्तन से छुटकारा मिल जाय और सृष्टि के अनवरत जन्म, वृद्धि, विनाश के अनिवार्य क्रम को समझ लिया जाय तो मनुष्य शान्त, सन्तुलित, स्थिर, सन्तुष्ट एवं सुखी रह सकता है। ऐसी देवोपम मनोभूमि पल-पल में स्वर्गीय जीवन की सुखद संवेदनाएं सम्मुख प्रस्तुत किये रह सकता है। चिन्तन में समाया हुआ माया विकार ही है जो समुद्र तट पर बैठे अज्ञानी बालक के, ज्वार से प्रसन्न और भाटा से अप्रसन्न होने की तरह हमें उद्विग्न बनाये रहता है।
मल-मूत्र की गठरी के ऊपर प्रकृति ने एक आकर्षक खोल चढ़ाया हुआ है ताकि वह घृणित पिटारा सर्वत्र दुर्गन्ध बखेरता न फिरे। लोग इस आवरण पर मुग्ध हो जाते हैं, रूप, यौवन पर लट्टू होते हैं। सौन्दर्य की शाश्वत प्यास सुकोमल पुष्प से लेकर बाल सुलभ भोलेपन तक से सर्वत्र सहज ही तृप्ति की जा सकती पर विकारी दृष्टि के साथ जुड़ी हुई कामुक लिप्सा नर-नारियों को बेतरह उद्विग्न करती रहती है और उन्हें न चलने योग्य मार्ग पर चलाती है। मूत्र त्याग के घृणित अंगों की तनिक सी खुजली न जाने किससे क्या-क्या नहीं कर लेती। यदि मोहान्ध दृष्टि का पर्दा उठ सका होता तो शारीरिक रूप, यौवन की—यौन लिप्सा की मदोन्मत्ता का नशा सहज ही उतर जाता और पंचभूतों से बने जड़-कलेवर के पीछे आत्मा की ज्योति जगमगाती दीखती। कामुकता का स्थान पवित्र प्रेम भावनाओं ने ग्रहण कर लिया होता और नर-नारी के बीच के सम्बन्ध प्रकृति और पुरुष की तरह एक दूसरे के पूरक बनकर श्रेय साधन में संलग्न रहे होते। आज का नारकीय दाम्पत्य-जीवन तब स्वर्गीय सुषमा बखेर रहा होता। ऐसे उच्च आदर्शों को आधार मानकर बनाये गये गृहस्थ तब स्वर्ग की प्रतिमूर्ति बनकर धरती को आनन्द, उल्लास से भर रहे होते और नर-रत्नों की पीढ़ियां सृजी जातीं। यह पिशाचिनी माया ही है जिसने रूप, सौन्दर्य को परखने का दृष्टि दोष उत्पन्न करके आत्मतत्व को तिरस्कृत और चमड़ी की चमक को गौरव प्रदान किया है।
अपना स्वरूप, अपना लक्ष्य, अपना कर्त्तव्य यदि मनुष्य समय सका होता तो उसका चिन्तन और कर्तृत्व अत्यन्त उच्चकोटि का होता ऐसे नर को नारायण कहा जाता और उसके चरण जहां भी पड़ते वहां धरती धन्य हो जाती। पर अज्ञान के आवरण को क्या कहा जाय जिसने हमें नर-पशु के स्तर पर देखने और उसी प्रकार की रीति-नीति अपनाने के लिए निकृष्टता के गर्त में धकेल दिया है। माया का यही आवरण हमें नारकीय यातनाएं सहन करते हुए रोता, कलपता जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करता है। संसार को जैसा कि हम देखते, समझते हैं वह पूर्व प्रचलित भ्रान्त धारणाओं पर और मस्तिष्क सहित इन्द्रियों के ज्ञान पर आधारित है। यदि हम एक बार इन दोनों आधारों की अप्रामाणिकता और अक्षमता को स्वीकार करलें तथा नये सिरे से अपने सम्बन्ध में, सम्बन्धित व्यक्तियों तथा पदार्थों के सम्बन्ध में समस्त विश्व ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में नये तर्क पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना आरंभ करें तो तथ्य बिलकुल दूसरे ही स्तर के सामने आवेंगे और वही प्रतिपादन सोलहों आने सत्य सिद्ध होगा जिसे वेदान्त दर्शन में निर्धारित किया गया है।
जिस प्रकार हर प्रभात को हम जगते हैं और हर रात को गहरी नींद में सोते हैं ठीक उसी प्रकार थोड़ी अधिक विस्तृत भूमिका में जनम और मरण की प्रक्रिया चलती रहती हैं। सूर्य हर दिन डूबता, उगता है। जीवन भी नियत अवधि में उत्पन्न और समाप्त होता रहता है। जिस तरह एक के बाद दूसरे दिन का लम्बा जीवनयापन चलता रहता है उसी प्रकार एक जन्म के बाद दूसरे जन्म की श्रृंखला चलती है। इसमें न कोई दुख की बात है न शोक की, न डर की। यह तथ्य यदि सामने प्रस्तुत रहे तो फिर जीवन की लम्बी श्रृंखला की योजना इस ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिये। यदि भावी जीवन को उज्ज्वल बनाने की सम्भावना सामने हो तो इसके लिये एक दिन के कष्ट, कठिनाई से व्यतीत करने की बात किसी को अखरती नहीं। ऐसी भूल भी कोई समझदार आदमी नहीं कर सकता कि एक दिन शौक-मौज मनाने के लिये कोई ऐसा अवांछनीय कार्य कर डाला जाय, जिसके लिए जीवन के शेष समस्त दिन विपत्ति में फंसकर व्यतीत करने पड़ें। मनुष्य-जीवन की भोजन व्यवस्था बनाते समय भी यदि यही रीति-नीति अपनाई जा सके तो समझना चाहिये कि अनन्त जीवनों की जुड़ी हुई श्रृंखला का स्वरूप समझ लिया गया। ऐसी दशा में न वस्तुओं से लोभ हो सकता है और न व्यक्तियों से मोह। तब केवल वस्तुओं के सदुपयोग और व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यपालन का भाव ही मन में उठता रह सकता है।
एक जन्म को ही पूरा जीवन मान बैठने से मनुष्य आज ही जी भरकर शौक-मौज करने के लिये आतुर होता है और भविष्य को अन्धकारमय बनाता है। यदि अनन्त जीवन में एक-एक जन्म को एक दिन की तरह नगण्य महत्व का माना जाय तो फिर विद्यार्थी के विद्याध्ययन, पहलवान और कृषक की तरह अनवरत कष्ट साधन करने के लिए उत्साह बना रहेगा और उज्ज्वल भविष्य की आस में आज की कठिनाइयों को तुच्छ माना जायेगा। पर होता ऐसा कहां है? इसका कारण वर्तमान को ही सब कुछ मान बैठने का मायावादी अज्ञान ही है। इसी में फंसकर मनुष्य दुर्बुद्धि अपनाता और पापकर्म करता है यदि माया का पर्दा हट जाय तो फिर बाल-क्रीड़ाओं को छोड़ कर वयस्कों और बुद्धिमानों जैसी गति-विधियां अपनाने की ही प्रवृत्ति बनेगी।
हम सब सराय में ठहरे हुये मुसाफिरों की तरह ही दिन व्यतीत कर रहे हैं। जल प्रवाह में बहते हुये तिनकों की तरह ही इकट्ठे हो गये हैं। जब मिल ही गये तो सराय के नियमों का सड़क पर चलने के कानूनों का क्षेत्र के नागरिक कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा, इस दृष्टि के विकसित होने पर यह अज्ञान हट जाता है कि कोई हमारा है या हम किसी के हैं। सब ईश्वर के हैं—और ईश्वर ही सबका हितू है। प्रत्येक प्राणी अपनी कर्म रज्जु में बंधा अपनी धुरी पर घूम रहा है। समय का परिपाक बहुतों को परस्पर जुड़ता और बिछुड़ता रहता है। यह सत्य यदि समझ में आ जाय तो न किसी के मोह बन्धन में बंधा जाय, न बांधा जाय। आत्मीयता के विस्तार द्वारा सम्पन्न होने वाला प्रेम हर किसी पर परिपूर्ण मात्रा में बखेरा जाय, पर उसमें विवेक का समुचित पुट रहे। परिवारी लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, पक्षपात और मोह के कारण उन्हें अनुचित लाभ देने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उससे हर किसी का घोर अहित होता है। मुफ्त में अनावश्यक सहायता पाकर परिवार के लोग मुफ्तखोर बनते हैं और अपने श्रम-साधनों से जो लोक-मंगल सम्भव था उससे समाज को वंचित रहना पड़ता है और व्यक्ति परमार्थ का कल्याणकारी लाभ लेने से वंचित रह जाता है। यह माया बन्धनों का परिणाम ही है जिसने मोह जाल में जकड़ कर विश्व हित को श्रेय साधना से वंचित करके पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने में भारी व्यवधान प्रस्तुत किया।
वस्तुएं हमें इसलिये मिलती हैं कि उनका श्रेष्ठतम सदुपयोग करके उनसे स्व-पर कल्याण की व्यवस्था बनाई जाय। साधन जड़ जगत के अंग हैं और वे रंग रूप बदलते हुए इस जगत की शोभा बढ़ाते रहने के लिए हैं। उन्हें अपने गर्व-गौरव का, विलास वैभव का आधार बनाकर संग्रह करते चलें। अहंकार का पोषण, तृष्णा की तुष्टि अथवा विलासिता के अभिवर्धन में धन को—शारीरिक, मानसिक विभूतियों को नियोजित रखा जाय तो उत्कृष्ट जीवन जी सकने का द्वार अवरुद्ध ही बना रहेगा। संकीर्ण और स्वार्थी जिन्दगी ही जियी जा सकेगी और इस कुचक्र में यह सुर-दुर्लभ अक्सर निरर्थक ही चला जायेगा।
शरीर और मन को अपना आपा मान बैठना और उसकी वासनाओं, तृष्णाओं की पूर्ति में इतना निमग्न हो जाना कि आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य पूरी तरह विस्मृत हो जाय, ये दूरदर्शितापूर्ण नहीं है। शारीरिक और मानसिक उपलब्धियों के लिये जितना श्रम किया जाता है और मनोयोग लगाया जाता है, जोखिम उठाया जाता है उतना ही विनियोग यदि आत्मोत्कर्ष के लिये—आत्मबल सम्पादन के लिये लगाया जा सके तो मनुष्य इसी जीवन में महामानव बन सकता है और उन विभूतियों को करतलगत कर सकता है जो देवदूतों में पाई जाती हैं। इतना उच्चकोटि का लाभ छोड़कर नगण्य-सी लिप्साओं में डूबे हुये न करने योग्य काम करना—उनके कटु-कर्म—परिपाक सहना, किसी विवेकवान के लिए उपयुक्त न होगा। किन्तु देखा जाता है कि अधिकांश व्यक्ति उचित छोड़कर अनुचित का, लाभ छोड़कर हानि का रास्ता अपनाते हैं इसे क्या कहा जाय? यह माया का खेल ही है। जिससे भ्रमित होकर मनुष्य जल में थल-थल में जल देखने की तरह हानि को लाभ और लाभ को हानि समझता है। अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारता है। माया विमुग्ध होकर ही मनुष्य अपने उच्च स्तर से अपनी दुर्बलताओं के कारण अधः पतित होता है और दुःख क्लेश भरा नरक भोगता है अन्यथा मनुष्य को इस विश्व के साथ सम्पर्क बनाकर सुखानुभूति प्राप्त कराने वाले जो तीन उपकरण मिले हैं यदि उनका ठीक तरह उपयोग किया जा सके तो जीवन अति सुन्दर और मधुर बन सकता है। इन तीन उपकरणों के नाम हैं। (1) अन्तरात्मा (2) मन (3) इन्द्रिय समूह।
इन्द्रियों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रिया में ही उन्हें पग-पग पर असाधारण सरसता अनुभव होती है। पेट भरने के लिए भोजन करना स्वाभाविक है। भगवान की कैसी महिमा है कि उसने दैनिक जीवन की शरीर यात्रा भर की नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया को कितना सरस बना दिया है। उपयुक्त भोजन करते हुये जीव को कितना रस मिलता है और चित्त को उस अनुभूति से कैसे प्रसन्नता होती है।
आंख का साधारण काम है वस्तुओं को देखना ताकि हमारी जीवन यात्रा ठीक तरह चलती रह सके। पर आंखों में कितनी अद्भुत विशेषता भर दी है कि वह रूप, सौन्दर्य, कौतुक, कौतूहल जैसी रस भरी अनुभूतियां ग्रहण करके चित्त को प्रफुल्लित बनाती हैं। संसार में उत्पादन, परिपुष्टि, विनाश का क्रम नितान्त स्वाभाविक है। मध्यवर्ती स्थिति में हर चीज तरुण होती है और सुन्दर लगती है। क्या पुष्प क्या मनुष्य हर किसी को तीनों स्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। मध्यकाल सौन्दर्य लगता है। वस्तुतः यह तीनों ही स्थितियां अपने क्रम, अपने स्थान और अपने समय पर सुन्दर हैं। पर आंखों को सुन्दर-असुन्दर का भेद करके मध्य स्थिति को सुन्दर समझने की कुछ अद्भुत विशेषता मिली है। फलस्वरूप जो कुछ उभरता हुआ विकसित, परिपुष्ट दीखता है सो सुन्दर लगता है। सुन्दर असुन्दर का तात्विक दृष्टि से यहां कुछ भी अस्तित्व नहीं है। पर हमारी अद्भुत आंखें ही हैं जो अपनी सौन्दर्यानुभूति वाली विशेषता के कारण हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्धित समीपवर्ती वस्तुओं में से सौन्दर्य वाला भाग देखतीं, आनन्द अनुभव करतीं, उल्लसित और पुलकित होती हैं। चित्त को प्रसन्न करती हैं।
इसी प्रकार जननेन्द्रिय की प्रक्रिया है। प्रजनन मक्खी मच्छरों, कीट-पतंगों, बीज अंकुरों में भी चलता रहता है। यह सृष्टि का सरल स्वाभाविक क्रम है पर हमारी जननेन्द्रिय में कैसा अजीब उल्लास सराबोर कर दिया है कि संभोग के क्षण ही नहीं—उसकी कल्पना भी मन के कोने-कोने में सिहरन पुलकन, उमंग और आतुरता भर देती है। तत्वतः बात कुछ भी नहीं है। दो शरीरों के दो अवयवों का स्पर्श—इसमें क्या अनोखापन है? क्या अद्भुतता है? क्या उपलब्धि है? फिर स्पर्श का कुछ प्रभाव हो भी तो उसकी कल्पना से किस प्रकार, क्यों, किस लिये चित्त को बेचैन करने वाली ललक पैदा होनी चाहिये? बात कुछ भी नहीं है। मात्र जननेन्द्रिय की बनावट में एक अद्भुत प्रकार की सरसता का समावेश मात्र है जो हमें सामान्य स्वाभाविक दाम्पत्य-जीवन के वास्तविक या काल्पनिक प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र में एक विचित्र प्रकार की रसानुभूति उत्पन्न करके—जीने भर के लिये प्रयुक्त हो सकने वाले जीवन को निरन्तर उमंगों से भरता रहता है।
ऊपर जीभ, आंख और जननेन्द्रिय की चर्चा हुई, कान और नाक के बारे में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। यहां पान भाग वाला इन्द्रिय समूह अपने साथ रसानुभूति की विलक्षणता इसलिये धारण किये हुये हैं कि सरस, स्वाभाविक सामान्य जीवन क्रम ऐसे ही नीरस ढर्रे का जीने भर के लिये मिला हुआ प्रतीत न हो वरन् उसमें हर घड़ी उत्साह, उल्लास, रस, आनन्द बना रहे और उसे उपलब्ध करते रहने के लिये जीवन की उपयोगिता, सार्थकता और सरसता का भान होता रहे। इन्द्रिय समूह हमें इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध है। यदि उनका उचित, संयमित, विवेकपूर्ण, व्यवस्था पूर्वक उपयोग किया जा सके, तो हमारा भौतिक सांसारिक जीवन पग-पग पर सरसता, आनन्द उपलब्ध करता रह सकता है।
दूसरा उपकरण मन इसलिए मिला है कि संसार में जो कुछ चेतन है उसके साथ अपनी चेतना का स्पर्श करके और भी ऊंचे स्तर की आनन्दानुभूति प्राप्त करे। इन्द्रियां जड़ शरीर से सम्बन्धित हैं। जड़ पदार्थों को स्पर्श करके—उस संसर्ग का सुख लूटती हैं। जड़ का जड़ से स्पर्श भी कितना सुखद हो सकता है, इस विचित्रता का अनुभव हमें इन्द्रियों के माध्यम से होता है। चेतन का चेतन के साथ, जीवधारी का जीवधारी के साथ स्पर्श—सम्पर्क होने से मित्रता, ममता, मोह, स्नेह, सद्भाव, घनिष्ठता, दया, करुणा, मुदिता जैसी अनुभूतियां होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष, घृणा जैसे भाव भी उत्पन्न होते हैं पर उनका अस्तित्व है इसीलिए कि मित्रता के वातावरण में सम्पर्क, संसर्ग का आनन्द बिखरता रहे, यदि अन्धकार न हो तो प्रकाश की विशेषता ही नष्ट हो जाय। वस्तुतः मन की बनावट दूसरों के सम्पर्क, सहयोग, स्नेह भावों के आदान-प्रदान का सुख प्राप्त करने में है। मेले-ठेलों में सभा सम्मेलनों में जाने की इच्छा इसीलिए उठती है उन जन संकुल स्थानों में व्यक्तियों की घनिष्ठता न सही समीपता का अदृश्य सुख तो अनायास मिलता ही है।
चूंकि इन्द्रिय सुख और जन सम्पर्क की घनिष्ठता में सहायक एक और नया माध्यम सभ्यता के विकास के साथ-साथ बनकर खड़ा हो गया है इसलिये अब प्रिय वह भी लगने लगा है—इस तीसरे मनुष्य कृत—आकर्षण तत्व का नाम है—धन में स्वभावतः कोई आकर्षण नहीं। इसमें इन्द्रिय समूह या मन को पुलकित करने वाली कोई सीधी क्षमता नहीं है। धातु के सिक्के या कागज के टुकड़े भला आदमी के लिए प्रत्यक्षतः क्यों आकर्षक हो सकते हैं। पर चूंकि वर्तमान समाज व्यवस्था के अनुसार धन के द्वारा इन्द्रिय सुख के साधन प्राप्त होते हैं। मैत्री भी सम्भव होती है। इसलिए धन भी प्रकारान्तर रूप से मन का प्रिय विषय बन गया। अस्तु धन की गणना भी सुखदायक माध्यमों से जोड़ ली गई है।
तीन शरीरों को जीवात्मा धारण किये हुए है। तीनों की तीन रसानुभूतियां हैं। ऊपर दो की चर्चा हो चुकी। स्थूल शरीर की सरसता-इन्द्रिय समूह के साथ जुड़ी हुई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे सुख इन्द्रियों द्वारा ही मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है। मन की सरसता मैत्री पर, जन सम्पर्क पर अवलम्बित है। परिवार मोह से लेकर समाज सम्बन्ध, नेतृत्व, सम्मिलन, उत्सव, आयोजन जैसे सम्पर्क परक अवसर मन को सुख देते हैं। घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने की सूक्ष्म सम्वेदना उत्पन्न करके वह समाज की अनेक हलचलों से भी अपने को बांध लेता है और उन घटना क्रमों में खट्टी-मीठी अनुभूतियां उपलब्ध करता है। उपन्यास, सिनेमा, अखबार रेडियो आदि मन को इसी आधार पर आकर्षित करते और प्रिय लगते हैं।
तीसरा रसानुभूति उपकरण है—अन्तरात्मा उसका कार्य क्षेत्र ‘कारण शरीर’ है। उसमें उत्कृष्टता, उत्कर्ष, प्रगति, गौरव की प्रवृत्ति रहती है जो उच्च भावनाओं के माध्यम से चरितार्थ होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता और सन्मार्गगामिता प्रखर होती रहे इसके लिए उसमें भी एक रसानुभूति विद्यमान है—उसका नाम है वर्चस्व, यश कामना, नेतृत्व, गौरव प्रदर्शन। उस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अगणित प्रकार की सफलतायें प्राप्त करता है ताकि वह स्वयं दूसरों की तुलना में अपने आपको श्रेष्ठ, पुरुषार्थी, पराक्रमी, बुद्धिमान अनुभव करके सुख प्राप्त करे और दूसरे लोग भी उसकी विशेषताओं, विभूतियों से प्रभावित होकर उसे यश, मान प्रदान करें।
संक्षेप में यह मनुष्य के तीन शरीरों की—तीन रसानुभूतियों की चर्चा हुई। हमारी अगणित योजनायें—इच्छा, आकांक्षायें गतिविधियां इन्हीं तीन मल प्रवृत्तियों के इर्द−गिर्द घूमती हैं। जो कुछ मनुष्य सोचता और करता है उसे तीन भोगों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान ने यह तीन उपहार जीवन को सरसता से भरा पूरा रखने के लिये दिये हैं। साथ ही उनका अस्तित्व इसलिये भी है कि व्यक्ति निरन्तर सक्रिय बना रहे। इन सुखानुभूतियों को प्राप्त करने के लिये उसके तीनों शरीर निरन्तर जुटे रहें। आलस्य, अवसाद की उदासीनता, नीरसता की स्थिति सामने आकर खड़ी न हो जाय और जीवन को आनन्द रहित भार रूप न बना दे। सक्रियता के आधार पर चल रहे सृष्टि क्रम को अवरुद्ध न करदे। अन्तरात्मा, मन और इन्द्रिय समूह को यदि सही मार्ग पर चलने का अवसर मिलता रहे तो जीवन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो सकता है। भूल मनुष्य की तब आरम्भ होती है जब वह इन तीनों रसानुभूतियों को अमर्यादित होकर—अनावश्यक मात्रा में—अति शीघ्र, बिना उचित मूल्य चुकाये प्राप्त करने के लिये आकुल, आतुर हो उठता है और लूट-खसोट की मनोवृत्ति अपनाकर अवांछनीय गतिविधियां अपना लेता है। विग्रह इसी से उत्पन्न होता है। पाप का कारण यही उतावली है। जीवन में अव्यवस्था और अस्त-व्यस्तता इसी से उत्पन्न होती। पतन इसी भूल का परिणाम है अपराधी, दुष्ट और घृणित बनने का कारण उन उपलब्धियों के लिये अनुचित मार्ग को अपनाना ही है। उतावला व्यक्ति आतुरता में विवेक खो बैठता है और औचित्य को भूलकर बहुत जल्दी—अधिक मात्रा में उपरोक्त सुखों को पाने के लिए असन्तुष्ट होकर एक प्रकार से उच्छृंखल हो उठता है। यह अमर्यादित स्थिति उसके लिए विपत्ति बनकर सामने आती है। सरल स्वाभाविक रीति से जो शान्ति पूर्वक मिल रहा था—मिलता रह सकता था—वह भी हाथ से चला जाता है और शारीरिक रोग, मानसिक उद्वेग—सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक अभाव आत्मिक अशान्ति के संकटों से घिरा हुआ जीवन नरक बन जाता है। अधिक के लिये उतावला मनुष्य सरसता स्वाभाविकता को भी खोकर उलटा शोक-संताप, कष्ट-क्लेश एवं अभाव, दारिद्र्य में फंस जाता है। आमतौर से मनुष्य यह भूल करते हैं। इसी भूल को माया, अज्ञान, अविद्या नामों से पुकारते हैं। यह भूल ही ईश्वर प्रदत्त पग-पग पर मिलती रहने वाली सरसता से वंचित करती है और इसी के कारण जीव ऊंचा उठने के स्थान पर नीचे गिरता है।
अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मनुष्य के चिन्तन और कर्तव्य को अमर्यादित न होने देने—अवांछनीयता न अपनाने के लिए आवश्यक विवेक और साहस उत्पन्न करता है मनुष्य अपने अस्तित्व को, लक्ष्य को व्यवहार को सही तरह समझे। सही मार्ग को अपनाकर सही परिणाम उपलब्ध करते हुए, प्रगति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ता चले। अपूर्णता से पूर्णता में विकसित हो। यही मार्गदर्शक करता—इसका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना आत्मविद्या का मूल प्रयोजन है।
यह स्मरण रखा जाना चाहिए मानव का निर्माण जड़ एवं चेतन दोनों के युग्म से हुआ है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक हमारी सभी इन्द्रियां क्रियाशील हैं और शरीर में हलचल है, लेकिन जिस क्षण चेतना या आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर मिट्टी का ढेला मात्र ही रहता है। कोई स्पन्दन, कोई क्रिया, कोई सार्थकता नहीं रह पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर एवं आत्मा का संयोग जहां जीवात्मा में विराट् शक्ति का स्रोत है वहां आत्मा से रहित शरीर का कोई मूल्य नहीं। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण हम अपने शरीर के सुख साधन जुटाने में खर्च करते हैं और इन्द्रियजन्य भोगों में मरते-खपते रहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय तक भी हम अपनी वासनाओं, तृष्णाओं एवं लिप्साओं को तुष्ट नहीं कर पाते।
जीवन के समग्र उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि हम शरीर एवं आत्मा दोनों के समन्वित विकास, परिष्कार एवं तुष्टि-पुष्टि का दृष्टिकोण बनावें। एक को ही सिर्फ विकसित करें और एक को उपेक्षित करें—ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता।