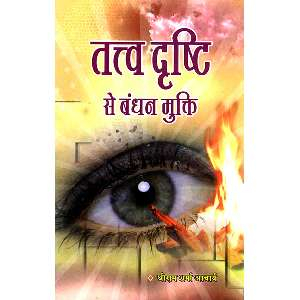तत्वदृष्टि से बंधन मुक्ति 
प्रत्यक्ष लगने पर भी सत्य कहां
Read Scan Version
जो कुछ हम देखते, जानते या अनुभव करते हैं—क्या वह सत्य है? इस प्रश्न का मोटा उत्तर हां में ही दिया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ सामने है, उसके असत्य होने का कोई कारण नहीं। चूंकि हमें अपने पर, अपनी इन्द्रियों और अनुभूतियों पर विश्वास होता है इसलिए वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो समझते हैं, उसे भी सत्य ही मानते हैं। इतने पर भी जब हम गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि इन्द्रियों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे बहुत अधूरे, अपूर्ण और लगभग असत्य ही होते हैं।
शास्त्रों और मनीषियों ने इसीलिए प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा अनुभव किये हुए को ही सत्य न मानने तथा तत्वदृष्टि विकसित करने के लिए कहा है। यदि सीधे सीधे जो देखा जाता व अनुभव किया जाता है उसे ही सत्य मान लिया जाय तो कई बार बड़ी दुःस्थिति बन जाती है। इस सम्बन्ध में मृगमरीचिका का उदाहरण बहुत पुराना है। रेगिस्तानी इलाके या ऊसर क्षेत्र में जमीन का नमक उभर कर ऊपर आ जाता है। रात की चांदनी में वह पानी से भरे तालाब जैसा लगता है। प्यासा मृग अपनी तृषा बुझाने के लिये वहां पहुंचता है और अपनी आंखों के भ्रम पर पछताता हुआ निराश वापस लौटता है। इन्द्र धनुष दीखता तो है पर उसे पकड़ने के लिये लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जल बिन्दुओं पर सूर्य की किरणों की चमक ही आंखों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है और हमें इन्द्र धनुष दिखाई पड़ता है उसका भौतिक अस्तित्व कहीं नहीं होता।
सिनेमा को ही लीजिये। पर्दे पर तस्वीर चलती-फिरती, बोलती, रोती-हंसती दीखती हैं। असम्भव जैसे जादुई दृश्य सामने आते हैं। क्या वह सारा दृश्यमान सत्य है। प्रति सेकेण्ड सोलह की गति से घूमने वाली अलग-अलग तस्वीरें हमारी आंखों की पकड़ परिधि से आगे निकल जाती हैं फलतः दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्थिर तस्वीरें चलती हुई मालूम पड़ती हैं। लाउडस्पीकर से शब्द अलग जगह निकलते हैं और तस्वीरें अलग जगह चलती हैं पर आंख कान इसी धोखे में रहते हैं कि तस्वीरों के मुंह से ही यह उच्चारण या गायन निकल रहे हैं।
प्रातःकालीन ऊषा और सायंकालीन सूर्यास्त के समय आकाश में जो रंग बिरंगा वातावरण छाया रहता है क्या वह यथार्थ है? वस्तुतः वहां कोई रंग नहीं होता यह प्रकाश किरणों के उतार चढ़ाव का दृष्टि संस्थान के साथ आंख मिचौनी ही है। आसमान नीला दीखता है पर वस्तुतः उसका कोई रंग नहीं है। पीला का रंग हो भी कैसे सकता है? आसमान को नीला बता कर हमारी आंखें धोखा खाती हैं और मस्तिष्क को भ्रमित करती हैं।
आंखों का काम मुख्यतया प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का स्वरूप समझना है। पर देखा जाता है कि उनकी आधी से ज्यादा जानकारी अवास्तविक होती है। कुछ उदाहरण देखिए। कारखानों की चिमनियों से धुओं निकलता रहता है। गौर करके उसका रंग देखिए वह अन्तर कई तरह का दिखाई देता रहता है। जब चिमनी की जड़ में पेड़, मकान आदि अप्रकाशित वस्तुएं हों तो धुआं काला दिखाई देगा पर यदि नीचे सूर्य का प्रकाश चमक रहा होगा तो वही धुआं भूरे रंग का दीखने लगेगा। लकड़ी, कोयला अथवा तेल जलने पर प्रकाश के प्रभाव से यह धुआं पीलापन लिये हुए दीखता है। वस्तुतः धुंए का कोई रंग नहीं होता। वह कार्बन की सूक्ष्म कणिकाओं अथवा तारकोल सदृश्य द्रव पदार्थों की बूंदों से बना होता है। इन से टकरा कर प्रकाश लौट जाता है और वे अंधेरी काले रंग की प्रतीत होती हैं।
रेल के इंजन में वायलर की निकास नली से निकलने वाली भाप निकलते समय तो नीली होती है पर थोड़ा ऊपर उठते ही संघतित हो जाने पर भाप के कणों का आकार बढ़ जाता है और वह श्वेत दिखाई देने लगती है।
जिन फैक्ट्रियों में घटिया कोयला जलता है उनका धुआं गहरा काला होता है और यदि उसमें से आर पार सूर्य को देखा जाय तो सूर्य गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। पानी के भीतर अगणित जीव-जन्तु विद्यमान रहते हैं पर खुली आंखों से उन्हें देख सकना संभव नहीं, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उन्हें देखा जा सकता है। आकाश में जितने तारे खुली आंखों से दिखाई पड़ते हैं उतने ही नहीं हैं। देखने की क्षमता से आगे भी अगणित तारे हैं जो विद्यमान रहते हुए भी आंखों के लिए अदृश्य ही हैं बढ़िया दूरबीनों से उन्हें देखा जाय तो दृश्य तारागणों की अपेक्षा लगभग दस गुने अदृश्य तारे दृष्टिगोचर होंगे।
परमाणु अणु की सत्ता को दूर सूक्ष्म दर्शक यन्त्रों से भी उसके यथार्थ रूप में देख सकना अभी भी सम्भव नहीं है। उसके अधिक स्थूल कलेवर की गणित के अध्यात्म पर विवेचना करके परमाणु और उसके अंग प्रत्यंगों का स्वरूप निर्धारण किया गया है। अणु संरचना के स्पष्टीकरण में जितनी सहायता उपकरणों ने की है उससे कहीं अधिक निष्कर्ष अनुमान पर निर्धारित गणित परक आधार पर निकाला जाना सम्भव हुआ है।
यथार्थता की तह तक पहुंचने के लिए हमें परख के आधार को अधिक विस्तृत करना पड़ेगा। इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठना भूल है। जो भौतिक प्रयोगशाला से प्रत्यक्ष हो सके वह सही है ऐसी बात भी तो नहीं है। ऊपर प्रकाश की आंख मिचौनी से रंगों की गलत अनुभूति होने की चर्चा की गई है। सत्य तक पहुंचने के लिए इन्हीं भोंड़े उपकरणों को परिपूर्ण मानकर चलेंगे तो अन्धकार में ही भटकते रहना पड़ेगा। किम्वदन्तियों और दन्तकथाओं के प्रतिपादनों से मुक्ति पाने के प्रयास में यदि इन्द्रिय ज्ञान की भोंडी भूल भुलैओं में भटक पड़े तो केवल पिंजड़ा बदला भर हुआ। स्थिति ज्यों त्यों बनी रही।
कुछ मोटी बातों को छोड़कर शेष सभी विषयों में हम जो कुछ देखते, जानते और अनुभव करते हैं उसके सम्बन्ध में यही मानते हैं कि वही सत्य है। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। अपने पर, अपनी इन्द्रियों और अनुभूतियों पर विश्वास होने के कारण वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो समझते हैं, उसे ही सत्य समझते हैं पर गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि हमारी मान्यतायें और अनुभूतियां हमें नितांत सत्य का बोध कराने में असमर्थ है। वे केवल पूर्ण मान्यताओं की अपेक्षा से ही कुछ अनुभूतियां करती है। यदि पूर्व मान्यतायें बदल जायें तो फिर अपने सारे निष्कर्ष या अनुभव भी बदलने पड़ेंगे।
मान्यताओं पर निर्भर निष्कर्ष
हमारा बुद्धि संस्थान केवल अपेक्षाकृत स्तर की जानकारियां दे सकने में ही समर्थ हैं। इतने से ही यदि सन्तोष होता हो तो यह कहा जा सकता है कि हम जो जानते या मानते हैं वह सत्य है। किन्तु अपनी मान्यताओं को ही यदि नितान्त सत्य की कसौटी पर कसने लगें तो प्रतीत होगा कि यह बुद्धि संस्थान ही बेतरह भ्रम ग्रसित हो रहा है फिर उसके सहारे नितान्त सत्य को कैसे प्राप्त किया जाय? यह एक ऐसा विकट प्रश्न है जो सुलझाये नहीं सुलझता।
वजन जिसके आधार पर वस्तुओं का विनिमय चल रहा है एक मान्यता प्राप्त तथ्य है। वजन के बिना व्यापार नहीं चल सकता। पर वजन सम्बन्धी हमारी मान्यताएं क्या सर्वथा सत्य हैं? इस पर विचार करते हैं तो पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। वजन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का जितना प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है उसे रोकने के लिए जितनी शक्ति लगानी पड़ेगी वही उसका वजन होता। तराजू बाटों के आधार पर हमें इसी बात का पता चलता है और उसी जानकारी को वजन मानते हैं, पर यह वजन तो घटता-बढ़ता रहता है। पृथ्वी पर जो वस्तु एक मन भारी है वह साड़े तीन मील ऊपर आकाश में उठ जाने पर आधी अर्थात् बीस सेर रह जायगी। इससे ऊपर उठने पर वह और हलकी होती चली जायगी। पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच एक जगह ऐसी आती है जहां पहुंचने पर उस वस्तु का वजन कुछ भी नहीं रहेगा। वहां अमर एक विशाल पर्वत भी रख दिया जाय तो वह बिना वजन का होने के कारण जहां का तहां लटका रहेगा। अन्य ग्रहों की गुरुता और आकर्षण शक्ति भिन्न है वहां पहुंचने पर अपनी पृथ्वी का भार माप सर्वथा अमान्य ठहराया जाय। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि वजन सापेक्ष है। किसी पूर्वमान्यता, स्थिति या तुलना के आधार पर ही उसका निर्धारण हो सकता है।
लोक व्यवहार की दूसरी इकाई है ‘गति’। वजन की तरह ही उसका भी महत्व है। गति ज्ञान के आधार पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के विभिन्न साधनों का मूल्यांकन होता है, पर देखना यह है कि ‘गति’ के सम्बन्ध में हमारे निर्धारण नितान्त सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं।
हम अपना कुर्सी पर बैठे लिख रहे हैं और जानते हैं कि स्थिर हैं। पर वस्तुतः एक हजार प्रति घण्टा की चाल से हम एक दिशा में उड़ते चले जा रहे हैं। पृथ्वी की यही चाल है। पृथ्वी पर बैठे होने के कारण हम उसी चाल से उड़ने के लिए विवश हैं। यद्यपि यह तथ्य हमारी इन्द्रियजन्य जानकारी की पकड़ में नहीं आता और निरन्तर स्थ्रिता प्रतीत होती है। पैरों से या सवारी से जितना चला जाता है, उसी को गति मानते हैं।
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए इस क्षण जहां हैं वहां वापिस 24 घण्टे बाद हो आ सकेंगे। पर यह सोचना भी व्यर्थ है क्योंकि पृथ्वी 666000 मील प्रति घण्टा की चाल से सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ी जा रही है। वह आकाश में जिस जगह है वहां लौटकर एक वर्ष बाद ही आ सकती है किन्तु यह मानना भी मिथ्या है क्योंकि सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी समेत अपने सौर परिवार के समस्त ग्रह उपग्रहों को लेकर और भी तीव्र गति से दौड़ता चला जा रहा है और वह महासूर्य अन्य किसी अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह सिलसिला न जाने कितनी असंख्य कड़ियों में जुड़ा होगा। अस्तु एक शब्द में यों कह सकते हैं कि जिस जगह आज हम हैं कम से कम इस जन्म में तो वहां फिर कभी लौटकर आ ही नहीं सकते। अपना आकाश छूटा तो सदा सर्वदा के लिए छूटेगा। इतने पर भी समझते यही रहते हैं कि जहां थे उसी क्षेत्र, देश या आकाश के नीचे कहीं जन्म भर बने रहेंगे।
स्थान की भांति गति की मात्रा भी भ्रामक है। दो रेलगाड़ियां समान पटरियों पर साथ-साथ दौड़ रही हों तो वे साथ-साथ हिलती-जुलती भर दिखाई पड़ेंगी दो मोटरें आमने सामने से आ रही हों और दोनों चालीस चालीस मील प्रति घण्टे की चाल से चल रही हों तो जब वे बराबर से गुजरेगी तो 80 मील की चाल का आभास होगा। जब कभी आमने सामने से आती हुई रेल गाड़ियां बराबर से गुजरती हैं तो दूना वेग मालूम पड़ता है, यद्यपि ये दोनों ही अपनी अपनी साधारण चाल से चल रही होती हैं। अपनी पृथ्वी जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है वही गति और दिशा अन्य ग्रह नक्षत्रों की रही होती तो आकाश पूर्णतया स्थिर दीखता। सूर्य तारे कभी न उगते न चलते न डूबते। जो जहां हैं वहीं सदा बना रहता। तब पूर्ण स्थिरता की अनुभूति होते हुये भी सब की गतिशीलता यथावत् बनी रहती।
गति सापेक्ष है। अन्तर कितनी ही तरह निकाला जा सकता है। सौ में से नब्बे निकालने पर दस बचते हैं। तीस में से बीस निकालने पर भी—पचास में से चालीस निकालने पर भी दस ही बचेंगे। अन्तर एक ही निकले इसके लिये अनेकों अंकों का अनेक प्रकार से उपयोग हो सकता है। इतनी भिन्नता रहने पर भी परिणाम में अन्तर न पड़ेगा। एक हजार का जोड़ निकालना हो तो कितने ही अंकों का कितनी ही प्रकार से वही जोड़ बन सकता है। गति मापने के बारे में भी यही बात है। भूतकाल के खगोल वेत्ता सूर्य को स्थिर मान कर यह गणित करते हैं। चन्द्र-ग्रहण, सूर्य ग्रहण सौर मण्डल के ग्रह-उपग्रहों का उदय-अस्त दिन मान, रात्रि मान आदि इसी आधार पर निकाला जाता रहा है। फिर भी वह बिलकुल सही बैठता रहा है। यद्यपि सूर्य को स्थिर मानकर चलने की मान्यता सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या आधार भी जब सत्य परिणाम प्रस्तुतः करते हैं तो फिर सत्य असत्य का भेद किस प्रकार किया जाय, यह सोचने पर बुद्धि थककर बैठ जाती है।
दिशा का निर्धारण भी लोक व्यवहार में आवश्यक है। इसके बिना भूगोल नक्शा, यातायात की कोई व्यवस्था ही न बनेगी। रेखा गणित में आड़ी, सीधी, तिरछी रेखाओं को ही आधार माना गया है। दिशा ज्ञान के बिना वायुयान और जलयानों के लिये निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकना ही सम्भव न होगा। पूर्व, पश्चिम आदि आठ और दो ऊपर नीचे की दशों दिशाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आधार हैं, पर ‘नितान्त सत्य’ का आश्रय लेने पर यह दिशा मान्यता भी लड़खड़ा कर भूमिसात् हो जाती है।
एक लम्बी नाली लगातार खोदते चले जायें तो प्रतीत होगा कि वह सीधी समतल जा रही है, पर वस्तुतः यह गोलाई में ही खुद रही है और वह क्रम चलता रहने पर खुदाई उसी स्थान पर आ पहुंचेगी जहां से वह आरम्भ हुई थी। रबड़ की गेंद पर बिलकुल सीधी रेखा खींचने पर भी वस्तुतः वह गोलाई में ही खिंच रही है, सीधी रेखा खींचने का मतलब उसके दोनों सिरों का अन्तर सदा बना रहना ही होना चाहिये, पर जब वे अन्ततः एक में आ मिलें तो फिर सीधी लकीर कहां हुई? कागज पर जमीन पर, या कहीं भी छोटी बड़ी सीधी लकीर खींची जाय वह कभी भी सीधी नहीं हो सकती। स्वल्प गोलाई अपने नाप साधनों से भले ही पकड़ में न आये, पर वस्तुतः वह गोल ही बन रही होगी। जिस भूमि को हम समतल समझते हैं वस्तुतः वह भी गोल है। समुद्र समतल दीखता है, पर उस पर चलने वाले जहाजों का मस्तूल ही पहले दीखता है इससे प्रतीत होता है कि पानी समतल प्रतीत होते हुये भी पृथ्वी के अनुपात में गोलाई लिये हुये है। जमीन पर खड़े होकर जमीन और आसमान मिलने वाला क्षितिज प्रायः 3 मील पर दिखाई पड़ता है पर यदि दो सौ फुट ऊंचाई पर चढ़ कर देखें तो वह बीस मील दूरी पर मिलता दिखाई देगा। यह बातें पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करती हैं। फिर भी मोटी बुद्धि से उसे गोल देख पाने का कोई प्रत्यक्ष साधन अपने पास नहीं हैं। वह समतल या ऊंची नीची दीखती है गोल नहीं। ऐसी दशा में हमारा दिशाज्ञान भी अविश्वस्त ही ठहरता है। चन्द्रमा हमसे ऊंचा है पर यदि चन्द्रतल पर जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पृथ्वी ऊपर आकाश में उदय होती है। सौर मण्डल से बाहर निकल कर कहीं आकाश में हम जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऊपर नीचे जैसे कोई दिशा नहीं है। दिशाज्ञान सर्वथा अपेक्षाकृत है। दिल्ली, लखनऊ से पश्चिम में बम्बई से पूर्व में, मद्रास से उत्तर में और हरिद्वार से दक्षिण में है। दिल्ली किस दिशा में है यह कहना किसी की तुलना अपेक्षा से ही सम्भव हो सकता है वस्तुतः वह दिशा विहीन है। समय की इकाई लोक व्यवहार में एक तथ्य है। घण्टा मिनट के सहारे ही दफ्तरों का खुलना बन्द होना रेलगाड़ियों का चलना रुकना—सम्भव होता है। अपनी सारी दिनचर्या समय के आधार पर ही बनती है। पर समय की मान्यता भी असंदिग्ध नहीं है। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय वही नहीं होता जो हम देखते या जानते हैं। जब हमें सूर्य उदय होते दीखता है उससे प्रायः 8।। मिनट पहले ही उग चुका होता है। उसकी किरणें पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है। अस्त होता जब दीखता है, उससे 8।। मिनट पूर्व ही वह डूब चुका होता है। आकाश में कितने ही तारे ऐसे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व अस्त हो चुके पर वे अभी तक हमें चमकते दीखते हैं। यह भ्रम इसलिये रहता है कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जब वे वस्तुतः अस्त हुये हैं उसकी जानकारी अब कहीं इतनी लम्बी अवधि के पश्चात हमें मिल रही है। सौर मण्डल के अपने ग्रहों के बारे में भी यही बात है, वे पंचांगों में लिखे समय से बहुत पहले या बाद में उदय तथा अस्त होते हैं।
जो तारा हमें सीध में दीखता है आवश्यक नहीं कि वह उसी स्थिति में है। प्रकाश की गति सर्वथा सीधी नहीं है। प्रकाश भी एक पदार्थ है और उसकी भी तोल है। एक मिनट में एक वर्ग मील जमीन पर सूर्य का जितना प्रकाश गिरता है उसका वजन प्रायः एक ओंस होता है। पदार्थ पर आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तारों का प्रकाश सौर मण्डल में प्रवेश करता है तो सूर्य तथा अन्य ग्रहों के आकर्षण के प्रभाव से लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा तिरछा होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। पर हमारी आंखें उसे सीधी धारा में आता हुआ ही अनुभव करती हैं। हो सकता है कि कोई तारा सूर्य या किसी अन्य ग्रह की ओट में छिपा बैठा हो पर उसका प्रकाश हमें आंखों की सीध में दीख रहा हो। इसी प्रकार ठीक सिर के ऊपर चमकने वाला तार वस्तुतः उस स्थान से बहुत नीचा या तिरछा भी हो सकता है। इस प्रकाश दिशा ही नहीं समय सम्बन्धी मान्यताएं भी निर्भ्रान्त नहीं हैं।
दार्शनिक विवेचनाओं से देश, काल का उल्लेख होता रहता है। उसे कोई मुल्क या घण्टा मिनट वाला समय नहीं समझ लेना चाहिये। यह पारिभाषिक शब्द है। वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई मोटाई को ‘देश’ कहा जाता है और उनके परिवर्तन को ‘काल’। आमतौर से वस्तुएं देश की अर्थात् लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर ही देखी जाती है जब कि उनकी व्याख्या विवेचना करते हुये काल का चौथा ‘आयाम’ भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। किन्तु गतियां और दिशाएं अनिश्चित भी हैं और भ्रामक भी। काल तो उन्हीं पर आश्रित है यदि आधार ही गड़बड़ा रहा है तो काल का परिमाण कैसे निश्चित हो। अस्तु वस्तुओं को तीन आयाम की अपेक्षा चार आयाम वाली भी कहा जाय तो भी बात बनेगी नहीं। वस्तुएं क्या हैं? उनका रूप, गुण, कर्म स्वभाव क्या है? यह कहते नहीं बनता क्योंकि उनके परमाणु जिस द्रुतगति से भ्रमण शील रहते हैं उस अस्थिरता को देखते हुये एक क्षण की गई व्याख्या दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जायगी।
कौन बड़ा कौन छोटा इसका निश्चय भी निःसंकोच नहीं किया जा सकता है। पांच फुट की लकड़ी छह फुट वाली की तुलना में छोटी है और चार फुट वाली की तुलना में बड़ी। एक फुट मोटाई वाले तने की तुलना में दो फुट वाला मोटा ‘अधिक’ है और दो फुट वाले की तुलना में एक फुट वाला पतला। वह वस्तुतः मोटा है या पतला ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तुलना बदलते ही यह छोटा और बड़ा होता—पतला और मोटा होता सहज ही बदल जायेगा।
कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन सुखी है कौन दुःखी, कौन सन्त है, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी, कौन सदाचारी है कौन दुराचारी, इसका निर्णय अनायास ही कर सकना असम्भव है। इस प्रकार का निर्धारण करने से पूर्व यह देखना होगा कि किस की तुलना में निर्णय किया जाय। नितान्त निर्धन की तुलना में वह धनी है जिसके पास पेट भरने के साधन हैं। किन्तु लक्षाधीश की तुलना में वह निर्धन ही है। जिसे दस कष्ट हैं उसकी तुलना में तीन कष्ट वाला सुखी है, पर एक कष्ट वाले की तुलना में वह भी दुःखी है। वस्तुतः कौन सुखी और कौन दुःखी हैं यह नहीं कहा जा सकता। डाकू की तुलना में चोर सहृदय है किन्तु उठाईगीरे की तुलना में वह भी अधिक दुष्ट है। एक सामान्य नागरिक की तुलना में उठाईगीरा भी दुष्ट है, जबकि वह सामान्य नागरिक भी सन्त की तुलना में पिछड़ा हुआ और गया-गुजरा है। सन्त भी किसी महा सन्त आत्मत्यागी शहीद की तुलना में हलका बैठेगा।
अपेक्षा से ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं तुलना ही एक मोटी कसौटी हमारे पास है जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिनके बारे में वह निर्धारण किया गया है वे वस्तुतः क्या हैं? इसका पता लगाना अपनी ज्ञानेन्द्रियों के लिये जिनमें मस्तिष्क भी सम्मिलित है, अति कठिन है। क्योंकि वे सभी अपूर्ण और सीमित हैं। कई अर्थों में तो उन्हें भ्रान्त भी कहा जा सकता है। सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरें चलती-फिरती दिखाई देती हैं वस्तुतः वे स्थिर होती हैं, उनके बदलने का क्रम ही इतना तेज होता है कि आंखें उसे ठीक तरह पकड़ नहीं पातीं और आकृतियों को ही हाथ-पैर हिलाती, बोलती, गाती समझ बैठती हैं।
अक्सर हमारी अनुभूतियां वस्तुस्थिति से सर्वथा उलटी होती हैं। इन्द्रियां अपूर्ण ही नहीं कई बार तो वे भ्रामक सूचनाएं देकर हमें ठगती भी हैं। उनके ऊपर निर्भर रहकर—प्रत्यक्षवाद को आधार मानकर शाश्वत सत्य को प्राप्त करना तो दूर समझ सकना भी सम्भव नहीं होता।
उदाहरण के लिये प्रकाश को ही लें। प्रकाश क्या है? उसे विद्युत चुम्बकीय लहरों का बवंडर ही कहा जा सकता है। वह कितना मन्द या तीव्र है यह तो उसकी मात्रा पर निर्भर है, पर उसकी चाल सदा एक-सी रहती है। एक सैकिण्ड में वह एक लाख छियासी हजार मील की गति से दौड़ते रहने वाला पदार्थ है। प्रकाश किरणों में सात रंग होते हैं! इन्हीं के सम्मिश्रण से हलके भारी अनेकानेक रंगों का सृजन होता है।
कोई रंग नहीं दुनिया में
यह बात कहने, सुनने और जानने, मानने में बड़ी विचित्र लगेगी कि संसार के किसी पदार्थ में कोई रंग नहीं है। हर वस्तु रंग रहित है। किन्तु यह विशेषता अवश्य है कि प्रकाश की किरणों में जो रंग है उनमें से किसी को स्वीकार करें किसी को लौटा दें। बस इसी कारण हमें विभिन्न वस्तुएं विभिन्न रंगों की दीखती हैं। पदार्थ जिस रंग की किरणों को अपने में सोखता नहीं वे उससे टकराकर वापिस लौटती हैं। वापसी में वे हमारी आंखों से टकराती हैं और हम उस टकराव को पदार्थ का अमुक रंग होने के रूप में अनुभव करते हैं। पौधे वस्तुतः हरे नहीं होते, उनका कोई रंग नहीं, हर पौधा सर्वथा बिना रंग का है, पर उसमें प्रकाश की हरी किरणें सोखने की शक्ति नहीं होती अस्तु वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वापिस लौटते हुये हमारी आंखों को इस भ्रम में डाल जाती हैं कि पौधे हरे होते हैं। हम उसी छलावे को शाश्वत सत्य मानते रहते हैं और प्रसंग आने पर पूरा जोर लगाकर यह सिद्ध करते रहते हैं कि पौधे निश्चित रूप से हरे होते हैं। कोई उससे भिन्न बात कहे तो हंसी उसी की बुद्धि पर आवेगी, भ्रांत और दुराग्रही उसी को कहेंगे। यह जानने और मानने का कोई मोटा आधार दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारी ही आंखें धोखा खा रही हैं—प्रकृति की जादूगरी, कलाबाजी हमें ही छल रही हैं। पेड़ का तो उदाहरण मात्र दिया गया। हर पदार्थ के बारे में हम रंगों के सम्बन्ध में ऐसे ही भ्रम जंजाल में जकड़े हुए हैं। जिन आंखों को प्रामाणिक मानते हैं, जिस मस्तिष्क की विवेचना पर विश्वास करते हैं यदि वही भ्रमग्रस्त होकर हमें झुठलाने लगें तो फिर हमारा ‘प्रत्यक्षवाद’ को तथ्य मानने का आग्रह बेतरह धूल धूसरित हो जाता है। हमारी दृष्टि में काला रंग सबसे गहरा रंग है और सफेद रंग कोई रंग नहीं है। पर यथार्थता इस मान्यता से सर्वथा उलटी है। किसी भी रंग का न दीखना काला रंग है और सातों रंगों सम्मिश्रण सफेद रंग। अंधेरा वस्तुतः ‘कुछ भी नहीं’ कहा जा सकता है जबकि वह घेर-घना छाया दीखता है और उसके कारण कुछ भी सूझ न पड़ने की स्थिति आ जाती है। वैशेषिक दर्शन ने अंधेरे को कोई पदार्थ मानने से इनकार किया है, जबकि दूसरे दार्शनिक उसे एक तत्व मानने का जोर-शोर से प्रतिपादन करते हैं। कालापन सभी प्रकाश किरणों को अपने भीतर सोख लेता है। फलतः हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है और अंधेरे में ठोकर खाते हैं—घनी कालिमा छाई देखते हैं।
किसी भी रंग की किरणें सोख सकने में जो पदार्थ सर्वथा असमर्थ हैं वे ही हमें सफेद दीखते हैं। कारण यह है उनसे टकरा कर तिरस्कृत प्रकाश तरंगें वापस लौटती हैं और उनके सातों रंगों का सम्मिश्रण हमारी आंखों को सफेद रंग के रूप में दीखता है। कैसी विचित्र, कैसी असंगत और कैसी भ्रम जंजाल भरी विडम्बना है यह। जिसे न उगलते बनता है न पीते। न स्वीकार करने को मन होता है अस्वीकार करने का साहस। अपने ही अपूर्ण उपकरणों पर क्षोभ व्यक्त न करते हुये मन मसोस कर बैठना पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धियों को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। हलका, भारी, गहरा, उथला कालापन भी एक पहेली है। अन्धकार कहीं या कभी बहुत गहरा होता है और कहीं या कभी उसमें हलकापन रहता है यह भी उतने अंशों में प्रकाश को सोखने न सोखने की क्षमता पर निर्भर रहता है। काले रंग में प्रकाश का सारा अंश सोख लेने की क्षमता का एक प्रमाण यह है कि वह धूप में अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी गरम होता है।
अब एक नया प्रश्न उभरता है कि प्रकाश किरणों में रंग कहां से आता है? इस स्थल पर उत्तर और भी विचित्र बन जाता है। प्रकाश लहरों की लम्बाई का अन्तर ही रंगों के रूप में दीखता है। वस्तुतः रंग नाम की कोई चीज समस्त विश्व में कहीं कुछ है ही नहीं। उसका अस्तित्व सर्वथा भ्रामक है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही प्रकाश हैं। इन तरंगों की लम्बाई अलग-अलग होती है। अस्तु उनका अनुभव हमारा मस्तिष्क भिन्न-भिन्न अनुभूतियों के साथ करता है। यह अनुभूति भिन्नता ही रंगों के रूप में विदित होती है। सात रंग तथा उनसे मिल-जुलकर बनने वाले अनेकानेक रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रकाश तरंगों की लम्बाई का मस्तिष्कीय अनुभूति के रूप में ही किया जा सकता है। रंगों की अपनी तात्विक सत्ता कुछ भी नहीं है।
आश्चर्य का अन्त इतने से ही नहीं हो जाता। रंगों की दुनिया बहुत बड़ी है उसे मेले में हमारी जान-पहचान बहुत थोड़ी-सी है। बाकी तो सब कुछ अनदेखा ही पड़ा है। लाल रंग की प्रकाश तरंगें एक इंच जगह में तेतीस हजार होती हैं जबकि कासनी रंग की सोलह हजार। इन्फ्रारेड तरंगें एक इंच में मात्र 80 ही होती हैं। इसके विपरीत रेडियो तरंगों की लम्बाई बीस मील से लेकर दो हजार मील तक पाई जाती है। यह अधिक लम्बाई की बात हुई। अब छोटाई की बात देखी जाय परा कासनी किरण एक इंच में बीस लाख तक होती हैं। एक्सरे किरणें एक इंच में पांच करोड़ से एक अरब तक पाई जाती हैं। गामा तरंगें एक इंच में 220 अरब। इतने पर भी इन सब की चाल एक जैसी है अर्थात् सैकिण्ड में वही एक लाख छियासी हजार मील।
अगर हम विदित प्रकाश किरणों को यन्त्रों की अपेक्षा खुली आंखों से देख सकने में समर्थ हो सके होते तो जिस प्रकाश एक सात रंगों का सप्तक हमें दीखता है उससे अतिरिक्त अन्यान्य ऐसे रंगों के जिनकी आज तो कल्पना कर सकना भी अपने लिए कठिन है 67 सप्तक और दीखते। 67×7=469 रंगों के सम्मिश्रण से कितने अधिक रंग बन जाते इसका अनुमान इसी से लगाया जाता है कि विज्ञान सात रंगों से ही हजारों प्रकार के हलके भारी रंग बने हुए दीखते हैं।
प्रातःकाल का अरुणोदय और लाल रंग का सूर्य निकलना इस रंग भ्रम जंजाल की एक झलक है। सूर्य वस्तुतः सफेद ही होता है, पर सवेरे वह सिर पर नहीं पूर्व में तिरछी स्थिति में होता है। इसलिए उसकी किरणों को बहुत लम्बा वायुमंडल पार करना पड़ता है। इस मार्ग में बहुत अधिक धूलि कण आड़े आते हैं। वे कण लाल रंग नहीं सोख पाते अस्तु वे किरणें हम तक चली आती हैं और सवेरे का उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई पड़ता है।
आंखें कितना अधिक धोखा खाती हैं और मस्तिष्क कितनी आसानी से बहक जाता है इसका एक उदाहरण रंगों की दुनिया में पहला पैर रखते ही विदित हो जाता है। अन्य विषयों में भी हमारी भ्रान्ति का ठिकाना नहीं। जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और लक्ष्य एक प्रकार से पूरी तरह विस्मृत कर दिया है और जड़ पदार्थों पर अपनी ही मान्यता को बखेर कर उन्हें प्रिय-अप्रिय के रूप में देखने की स्थिति को संसार से मिलने वाले सुख-दुख मान लिया है। आत्म-ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि यदि मिल सके तो पता लगेगा कि हम अज्ञान, माया और भ्रम के जिस जंजाल में फंसे हुए हैं उनसे निकले बिना सत्य के दर्शन नहीं हो सकते और सत्य के बिना सुख नहीं मिल सकता।
वेदान्त दर्शन संसार को माया बताता है और संसार को स्वप्न कहता है इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ दीखता है उसका अस्तित्व ही नहीं अथवा जो सामने है वह झूठ है। वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति में वे सत्य भी हैं। यदि ऐसा न होता तो कर्म फल क्यों मिलते? पुण्य और तप तितीक्षा करने की क्या आवश्यकता होती। कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या अन्त होता? धर्मकृत्यों की क्या उपयोगिता रह जाती? और पाप कर्मों से डरने बचने की क्या आवश्यकता रहती?
माया का अर्थ वेदान्त ने इस अर्थ में किया है जिसमें जो भाषित होता हो वह तत्वतः यथार्थ न हो। जगत को इसी स्थिति में—इसी स्तर का माना गया है। वह जैसा कुछ प्रतीत होता है, क्या वह वैसा ही है? इस प्रश्न पर जब गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि संसार में जो कुछ हम इन्द्रियों द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं वह यथार्थ में वैसा ही नहीं होता। इन्द्रिय छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क को होने वाली अनुभूतियों का नाम ही जानकारी तभी सत्य हो सकती है जब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को सही रूप में इन्द्रियां समझ सकें। यदि वे धोखा खाने लगें तो मस्तिष्क गलत अनुभव करेगा और वस्तुस्थिति उलटी दिखाई पड़ने लगेगी।
नशा पी लेने पर मस्तिष्क और इन्द्रियों का संबंध लड़खड़ा जाता है, फलस्वरूप कुछ का कुछ अनुभव होता है शराब के नशे में धुत्त व्यक्ति जैसा कुछ सोचता, समझता, देखता अनुभव करता है वह यथार्थता से बहुत भिन्न होता है। और भी ऊंचे नशे इस उन्मत्तता की स्थिति को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। डी. एलस्केस. ए. सरीखे नवीन नशे तो इतने तीव्र हैं कि उनके सेवन के उपरान्त ऐसे विचित्र अनुभव मस्तिष्क को होते हैं जिनकी यथार्थता के साथ कोई संगति नहीं होती।
साधारणतया दैनिक जीवन में भी अधिकांश अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें यथार्थ नहीं कहा जा सकता। सिनेमा के पर्दे पर जो दीखता है सही कहां है? एक के बाद एक आने वाली अलग-अलग तस्वीरें इतनी तेजी से घूमती हैं कि उस परिवर्तन को आंखें ठीक तरह समझ नहीं पातीं और ऐसा भ्रम होता है मानो फिल्म में पात्र चल फिर रहे हैं। लाउडस्पीकर से शब्द अलग अन्यत्र निकलते हैं और पर्दे पर तस्वीर के होठ अलग चलते हैं पर दर्शकों को ऐसा ही आभास होता रहता है मानो अभिनेताओं के मुख से ही वार्तालाप एवं संगीत निकल रहा है। प्रकाश की विरलता और सघनता भर पर्दे पर उतरती है पर उसी से पात्रों एवं दृश्यों का स्वरूप बन जाता है और मस्तिष्क ऐसा अनुभव करता है मानो यथार्थ ही वह घटना क्रम घटित हो रहा है।
सिनेमा के दृश्य क्रम को देखकर आने वाला यह नहीं अनुभव करता कि उसे यांत्रिक जाल जंजाल में ढाई तीन घंटे उलझा रहना पड़ा है। उसे जो दुखद-सुखद रोचक भयानक अनुभूतियां उतने समय होती रही हैं वे सर्वथा भ्रान्त थीं। सिनेमा हाल में कोई घटना क्रम नहीं घटा। कोई प्रभावोत्पादक परिस्थिति नहीं बनी केवल प्रकाश यन्त्र या ध्वनि यन्त्र अपने-अपने ढंग की कुछ हरकतें भी करते रहे। इतने भर से दर्शक अपने सामने अति महत्वपूर्ण घटना क्रम उपस्थित होते का आभास करता रहा, इतना ही नहीं उससे हर्षातिरेक एवं अश्रुपात जैसी भाव भरी मनःस्थिति में भी बना रहा। इस इन्द्रिय भ्रम को माया कहा जाता है। मोटी दृष्टि से यह माया सत्य है। यदि सत्य न होती तो फिल्म उद्योग, सिनेमा हाल, उसमें युक्त हुए यन्त्र, दर्शकों की भीड़ उनकी अनुभूति आदि का क्या महत्व रह जाता? थोड़ी विवेचनात्मक गहराई से देखा जाय तो यह यन्त्रों की कुशलता और वस्तुस्थिति को समझ न सकने को नेत्र असमर्थता के आधार पर इस फिल्म दर्शन को मायाचार भी कह सकते हैं। दोनों ही तथ्य अपने अपने ढंग से सही हैं। संसार चूंकि हमारे सामने खड़ा है, उसके घटना क्रम को प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए वह सही है किन्तु गहराई में प्रवेश करने पर वे दैनिक अनुभूतियां नितान्त भ्रामक सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन्हें भ्रम, स्वप्न या माया कहना भी अत्युक्ति नहीं है।
स्पष्ट है सभी दृश्य पदार्थ एक विशेष प्रकार के परमाणुओं का एक विशेष प्रकार का संयोग मात्र हैं। प्रत्येक परमाणु अत्यन्त तीव्र गति से गतिशील है। इस प्रकार हर पदार्थ अपनी मूल स्थिति में आश्चर्यजनक तीव्र गति से हरकत कर रहा है। पर खुली आंखें यह सब कुछ देख नहीं पातीं और वस्तुएं सामने जड़वत् स्थिर खड़ी मालूम पड़ती है। ऐसा ही अपनी पृथ्वी के बारे में भी होता है। भूमण्डल अत्यन्त तीव्र गति से (1) अपनी धुरी पर (2) सूर्य की परिक्रमा के लिए अपनी कक्षा पर (3) सौर मंडल सहित महासूर्य की परिक्रमा के पथ पर (4) घूमता हुआ लट्टू जिस तरह इधर उधर लहकता रहता है उस तरह लहकते रहने के क्रम पर (5) ब्रह्माण्ड के फलते फूलते जाने की प्रक्रिया के कारण अपने यथार्थ आकाश स्थान को छोड़ कर फैलता स्थान पकड़ते जाने की व्यवस्था पर—निरन्तर एक साथ पांच प्रकार की चालें चलती रहती हैं। इस उद्धत नृत्य को हम तनिक भी अनुभव नहीं करते और देखते हैं कि जन्म से लेकर मरण काल तक धरती अपने स्थान पर जड़वत् जहां की तहां पड़ी रही है। आंखों के द्वारा मस्तिष्क को इस सम्बन्ध में जो जानकारी दी जाती है और जैसी कुछ मान्यता आमतौर से बनी रहती है उसका विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होगा कि हम भ्रम अज्ञान की स्थिति में पड़े रहते हैं और कुछ का कुछ अनुभव करते रहते हैं, यह माया ग्रस्त स्थिति कही जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी।
जल में सूर्य चन्द्र के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं और लगता है कि पानी में प्रकाश पिण्ड जगमगा रहे हैं। हल लहर पर प्रतिबिम्ब पड़ने से हर लहर पर एक चन्द्रमा नाचता थिरकता मालूम पड़ता है। रेल में बैठने वाले देखते हैं कि वे अपने स्थान पर स्थिर बैठे हैं केवल बाहर तार के खंभे और पेड़ आदि भार रहे हैं। क्या यह अनुभूतियां सत्य हैं। रात्रि को स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ने वाला घटना क्रम यथार्थ मालूम पड़ता है। देखते समय दुख-सुख भी होता है। यदि यथार्थ में संदेह होता तो कई बार मुख से कुछ शब्द निकल पड़ना—स्वप्नदोष आदि हो जाने की बात क्यों होती? जागने पर स्पष्ट हो जाता है कि जो अपना देखा गया था उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं था। केवल कल्पनाओं की उड़ान को निद्रित मस्तिष्क ने यथार्थता अनुभव कर लिया। उतने समय की मूर्छित मनःस्थिति अपने को भ्रम जंजाल में फंसाये रह कर बेसिर पैर की उड़ानों में उड़ाती रही।
अंधेरे में झाड़ी भूत जैसी लगती है—रस्सी का टुकड़ा सांप प्रतीत होता है, मरीचिकाएं थल में जल का और जल में थल का भान कराती हैं। यथार्थता से सर्वथा भिन्न अनुभूतियों का होना कोई अनहोनी बात नहीं है। आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने वाले वायुयान छोटे पक्षी जैसे लगते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुने बड़े और अपने सूर्य से हजारों गुने अधिक चमकदार तारागण नन्हे से दीपक की तरह टिमटिमाते दीखते हैं। क्या यह सारे दृश्य यथार्थ में वैसे ही हैं जैसे कि आंखें हमें अनुभव कराती हैं? आंखों की तरह ही अन्य इन्द्रियों की बात है। वे एक सीमा तक ही वस्तुस्थिति का ज्ञान कराती हैं और जो बताती जताती हैं उसमें से भी अधिकांश भ्रान्त होता है। बुखार आने पर गर्मी की ऋतु में शीत का और शीत में गर्मी का अनुभव होता है। मुंह का जायका खराब होने पर हर चीज कड़वी लगती है। जुकाम हो जाने पर चारों ओर बदबू का अनुभव होता है। पीलिया रोग होने पर आंखें पीली हो जाती हैं और हर चीज पीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्या यह अनुभूतियां सही होती हैं?
जिस वस्तु का जैसा स्वाद प्रतीत होता है वह वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य को जो नीम के पत्ते कडुए लगते हैं, वे ऊंट को भी वैसे ही क्यों न लगते, वह उन्हें रुचि पूर्वक स्वादिष्ट पदार्थों की तरह क्यों खाता? खाद्य पदार्थों का स्वाद हर प्राणी की जिह्वा से निकलते रहने वाला अलग अलग स्तर के रसों तथा मुख के ज्ञान तन्तुओं की बनावट पर निर्भर है। भोजन मुंह में गया—वहां के रसों का सम्मिश्रण हुआ और उस मिलाप की जैसी कुछ प्रतिक्रिया मस्तिष्क पर हुई उसी का नाम स्वाद की अनुभूति है। खाद्य पदार्थ की वास्तविक रासायनिक स्थिति इस स्वाद अनुभूति से सर्वथा भिन्न है। जो कुछ चखने पर अनुभव होता है वह यथार्थता नहीं है।
शरीर विज्ञानी जानते हैं कि काया का निर्माण अरबों खरबों कोशिकाओं के सम्मिलन से हुआ है। उनमें से प्रतिक्षण लाखों मरती हैं और नई उपजती हैं। यह क्रम बराबर चलता रहता है और थोड़े ही दिनों में, कुछ समय पूर्व वाली समस्त कोशिकाएं मर जाती हैं और उनका स्थान नई ग्रहण कर लेती हैं। इस तरह एक प्रकार से शरीर का बार-बार काया कल्प होता रहता है। पुरानी वस्तु एक भी नहीं रहती उनका स्थान नये जीव कोष ग्रहण कर लेते हैं। देह के भीतर एक प्रकार श्मशान जलता रहता है और प्रसूति ग्रह में प्रजनन की धूम मची रहती है। इतनी बड़ी हलचल का हमें तनिक भी बोध नहीं होता और लगता है देह जैसी की तैसी रहती है। जिन इन्द्रियों के सहारे हम अपना काम चलाते हैं उनमें इतना भी दम नहीं होता कि बाहरी वस्तुस्थिति बनाना तो दूर अपने भीतर की इतनी महत्वपूर्ण हलचलों का तो आभास दे सकें। ऐसी इन्द्रियों के आधार पर यथार्थ जानकारी का दावा कैसे किया जाय? जिस मस्तिष्क को अपने कार्यक्षेत्र-शरीर के भीतर होने वाले रोगों में क्या स्थिति बनी हुई है, इतना तक ज्ञान नहीं है और घर की बात को बाहर वालों से पूछना पड़ता है वैद्य डाक्टरों का दरवाजा खट-खटाना पड़ता है, उस मस्तिष्क पर यह भरोसा कैसे किया जाय कि वह इस ज्ञान का वस्तुस्थिति में हमें सही रूप में अवगत करा देगा।
ज्ञान जीवन का प्राण है। पर वह होना यथार्थ स्तर का चाहिए। यदि कुछ का कुछ समझा जाय, उलटा देखा और जाना जाय, भ्रम विपर्यय हमारी जानकारियों का आधार बन जाय तो समझना चाहिए यह ज्ञान प्रतीत होने वाली चेतना वस्तुतः अज्ञान ही है। उसमें जकड़े रहने पर हमें विविध विधि त्रास ही उठाने पड़ेंगे, पग-पग पर ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसी स्थिति को माया कहते हैं। माया कोई बाहरी संकट नहीं, मात्र भीतरी भ्रान्ति भरी मनःस्थिति ही है, यदि उसे सुधार लिया जाय, तो समझना चाहिए माया के बन्धनों से मुक्ति मिल गई यह मुक्ति वस्तुतः हर किसी के करतलगत है।
शास्त्रों और मनीषियों ने इसीलिए प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा अनुभव किये हुए को ही सत्य न मानने तथा तत्वदृष्टि विकसित करने के लिए कहा है। यदि सीधे सीधे जो देखा जाता व अनुभव किया जाता है उसे ही सत्य मान लिया जाय तो कई बार बड़ी दुःस्थिति बन जाती है। इस सम्बन्ध में मृगमरीचिका का उदाहरण बहुत पुराना है। रेगिस्तानी इलाके या ऊसर क्षेत्र में जमीन का नमक उभर कर ऊपर आ जाता है। रात की चांदनी में वह पानी से भरे तालाब जैसा लगता है। प्यासा मृग अपनी तृषा बुझाने के लिये वहां पहुंचता है और अपनी आंखों के भ्रम पर पछताता हुआ निराश वापस लौटता है। इन्द्र धनुष दीखता तो है पर उसे पकड़ने के लिये लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जल बिन्दुओं पर सूर्य की किरणों की चमक ही आंखों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है और हमें इन्द्र धनुष दिखाई पड़ता है उसका भौतिक अस्तित्व कहीं नहीं होता।
सिनेमा को ही लीजिये। पर्दे पर तस्वीर चलती-फिरती, बोलती, रोती-हंसती दीखती हैं। असम्भव जैसे जादुई दृश्य सामने आते हैं। क्या वह सारा दृश्यमान सत्य है। प्रति सेकेण्ड सोलह की गति से घूमने वाली अलग-अलग तस्वीरें हमारी आंखों की पकड़ परिधि से आगे निकल जाती हैं फलतः दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्थिर तस्वीरें चलती हुई मालूम पड़ती हैं। लाउडस्पीकर से शब्द अलग जगह निकलते हैं और तस्वीरें अलग जगह चलती हैं पर आंख कान इसी धोखे में रहते हैं कि तस्वीरों के मुंह से ही यह उच्चारण या गायन निकल रहे हैं।
प्रातःकालीन ऊषा और सायंकालीन सूर्यास्त के समय आकाश में जो रंग बिरंगा वातावरण छाया रहता है क्या वह यथार्थ है? वस्तुतः वहां कोई रंग नहीं होता यह प्रकाश किरणों के उतार चढ़ाव का दृष्टि संस्थान के साथ आंख मिचौनी ही है। आसमान नीला दीखता है पर वस्तुतः उसका कोई रंग नहीं है। पीला का रंग हो भी कैसे सकता है? आसमान को नीला बता कर हमारी आंखें धोखा खाती हैं और मस्तिष्क को भ्रमित करती हैं।
आंखों का काम मुख्यतया प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का स्वरूप समझना है। पर देखा जाता है कि उनकी आधी से ज्यादा जानकारी अवास्तविक होती है। कुछ उदाहरण देखिए। कारखानों की चिमनियों से धुओं निकलता रहता है। गौर करके उसका रंग देखिए वह अन्तर कई तरह का दिखाई देता रहता है। जब चिमनी की जड़ में पेड़, मकान आदि अप्रकाशित वस्तुएं हों तो धुआं काला दिखाई देगा पर यदि नीचे सूर्य का प्रकाश चमक रहा होगा तो वही धुआं भूरे रंग का दीखने लगेगा। लकड़ी, कोयला अथवा तेल जलने पर प्रकाश के प्रभाव से यह धुआं पीलापन लिये हुए दीखता है। वस्तुतः धुंए का कोई रंग नहीं होता। वह कार्बन की सूक्ष्म कणिकाओं अथवा तारकोल सदृश्य द्रव पदार्थों की बूंदों से बना होता है। इन से टकरा कर प्रकाश लौट जाता है और वे अंधेरी काले रंग की प्रतीत होती हैं।
रेल के इंजन में वायलर की निकास नली से निकलने वाली भाप निकलते समय तो नीली होती है पर थोड़ा ऊपर उठते ही संघतित हो जाने पर भाप के कणों का आकार बढ़ जाता है और वह श्वेत दिखाई देने लगती है।
जिन फैक्ट्रियों में घटिया कोयला जलता है उनका धुआं गहरा काला होता है और यदि उसमें से आर पार सूर्य को देखा जाय तो सूर्य गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। पानी के भीतर अगणित जीव-जन्तु विद्यमान रहते हैं पर खुली आंखों से उन्हें देख सकना संभव नहीं, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उन्हें देखा जा सकता है। आकाश में जितने तारे खुली आंखों से दिखाई पड़ते हैं उतने ही नहीं हैं। देखने की क्षमता से आगे भी अगणित तारे हैं जो विद्यमान रहते हुए भी आंखों के लिए अदृश्य ही हैं बढ़िया दूरबीनों से उन्हें देखा जाय तो दृश्य तारागणों की अपेक्षा लगभग दस गुने अदृश्य तारे दृष्टिगोचर होंगे।
परमाणु अणु की सत्ता को दूर सूक्ष्म दर्शक यन्त्रों से भी उसके यथार्थ रूप में देख सकना अभी भी सम्भव नहीं है। उसके अधिक स्थूल कलेवर की गणित के अध्यात्म पर विवेचना करके परमाणु और उसके अंग प्रत्यंगों का स्वरूप निर्धारण किया गया है। अणु संरचना के स्पष्टीकरण में जितनी सहायता उपकरणों ने की है उससे कहीं अधिक निष्कर्ष अनुमान पर निर्धारित गणित परक आधार पर निकाला जाना सम्भव हुआ है।
यथार्थता की तह तक पहुंचने के लिए हमें परख के आधार को अधिक विस्तृत करना पड़ेगा। इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठना भूल है। जो भौतिक प्रयोगशाला से प्रत्यक्ष हो सके वह सही है ऐसी बात भी तो नहीं है। ऊपर प्रकाश की आंख मिचौनी से रंगों की गलत अनुभूति होने की चर्चा की गई है। सत्य तक पहुंचने के लिए इन्हीं भोंड़े उपकरणों को परिपूर्ण मानकर चलेंगे तो अन्धकार में ही भटकते रहना पड़ेगा। किम्वदन्तियों और दन्तकथाओं के प्रतिपादनों से मुक्ति पाने के प्रयास में यदि इन्द्रिय ज्ञान की भोंडी भूल भुलैओं में भटक पड़े तो केवल पिंजड़ा बदला भर हुआ। स्थिति ज्यों त्यों बनी रही।
कुछ मोटी बातों को छोड़कर शेष सभी विषयों में हम जो कुछ देखते, जानते और अनुभव करते हैं उसके सम्बन्ध में यही मानते हैं कि वही सत्य है। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। अपने पर, अपनी इन्द्रियों और अनुभूतियों पर विश्वास होने के कारण वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो समझते हैं, उसे ही सत्य समझते हैं पर गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि हमारी मान्यतायें और अनुभूतियां हमें नितांत सत्य का बोध कराने में असमर्थ है। वे केवल पूर्ण मान्यताओं की अपेक्षा से ही कुछ अनुभूतियां करती है। यदि पूर्व मान्यतायें बदल जायें तो फिर अपने सारे निष्कर्ष या अनुभव भी बदलने पड़ेंगे।
मान्यताओं पर निर्भर निष्कर्ष
हमारा बुद्धि संस्थान केवल अपेक्षाकृत स्तर की जानकारियां दे सकने में ही समर्थ हैं। इतने से ही यदि सन्तोष होता हो तो यह कहा जा सकता है कि हम जो जानते या मानते हैं वह सत्य है। किन्तु अपनी मान्यताओं को ही यदि नितान्त सत्य की कसौटी पर कसने लगें तो प्रतीत होगा कि यह बुद्धि संस्थान ही बेतरह भ्रम ग्रसित हो रहा है फिर उसके सहारे नितान्त सत्य को कैसे प्राप्त किया जाय? यह एक ऐसा विकट प्रश्न है जो सुलझाये नहीं सुलझता।
वजन जिसके आधार पर वस्तुओं का विनिमय चल रहा है एक मान्यता प्राप्त तथ्य है। वजन के बिना व्यापार नहीं चल सकता। पर वजन सम्बन्धी हमारी मान्यताएं क्या सर्वथा सत्य हैं? इस पर विचार करते हैं तो पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। वजन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का जितना प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है उसे रोकने के लिए जितनी शक्ति लगानी पड़ेगी वही उसका वजन होता। तराजू बाटों के आधार पर हमें इसी बात का पता चलता है और उसी जानकारी को वजन मानते हैं, पर यह वजन तो घटता-बढ़ता रहता है। पृथ्वी पर जो वस्तु एक मन भारी है वह साड़े तीन मील ऊपर आकाश में उठ जाने पर आधी अर्थात् बीस सेर रह जायगी। इससे ऊपर उठने पर वह और हलकी होती चली जायगी। पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच एक जगह ऐसी आती है जहां पहुंचने पर उस वस्तु का वजन कुछ भी नहीं रहेगा। वहां अमर एक विशाल पर्वत भी रख दिया जाय तो वह बिना वजन का होने के कारण जहां का तहां लटका रहेगा। अन्य ग्रहों की गुरुता और आकर्षण शक्ति भिन्न है वहां पहुंचने पर अपनी पृथ्वी का भार माप सर्वथा अमान्य ठहराया जाय। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि वजन सापेक्ष है। किसी पूर्वमान्यता, स्थिति या तुलना के आधार पर ही उसका निर्धारण हो सकता है।
लोक व्यवहार की दूसरी इकाई है ‘गति’। वजन की तरह ही उसका भी महत्व है। गति ज्ञान के आधार पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के विभिन्न साधनों का मूल्यांकन होता है, पर देखना यह है कि ‘गति’ के सम्बन्ध में हमारे निर्धारण नितान्त सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं।
हम अपना कुर्सी पर बैठे लिख रहे हैं और जानते हैं कि स्थिर हैं। पर वस्तुतः एक हजार प्रति घण्टा की चाल से हम एक दिशा में उड़ते चले जा रहे हैं। पृथ्वी की यही चाल है। पृथ्वी पर बैठे होने के कारण हम उसी चाल से उड़ने के लिए विवश हैं। यद्यपि यह तथ्य हमारी इन्द्रियजन्य जानकारी की पकड़ में नहीं आता और निरन्तर स्थ्रिता प्रतीत होती है। पैरों से या सवारी से जितना चला जाता है, उसी को गति मानते हैं।
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए इस क्षण जहां हैं वहां वापिस 24 घण्टे बाद हो आ सकेंगे। पर यह सोचना भी व्यर्थ है क्योंकि पृथ्वी 666000 मील प्रति घण्टा की चाल से सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ी जा रही है। वह आकाश में जिस जगह है वहां लौटकर एक वर्ष बाद ही आ सकती है किन्तु यह मानना भी मिथ्या है क्योंकि सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी समेत अपने सौर परिवार के समस्त ग्रह उपग्रहों को लेकर और भी तीव्र गति से दौड़ता चला जा रहा है और वह महासूर्य अन्य किसी अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह सिलसिला न जाने कितनी असंख्य कड़ियों में जुड़ा होगा। अस्तु एक शब्द में यों कह सकते हैं कि जिस जगह आज हम हैं कम से कम इस जन्म में तो वहां फिर कभी लौटकर आ ही नहीं सकते। अपना आकाश छूटा तो सदा सर्वदा के लिए छूटेगा। इतने पर भी समझते यही रहते हैं कि जहां थे उसी क्षेत्र, देश या आकाश के नीचे कहीं जन्म भर बने रहेंगे।
स्थान की भांति गति की मात्रा भी भ्रामक है। दो रेलगाड़ियां समान पटरियों पर साथ-साथ दौड़ रही हों तो वे साथ-साथ हिलती-जुलती भर दिखाई पड़ेंगी दो मोटरें आमने सामने से आ रही हों और दोनों चालीस चालीस मील प्रति घण्टे की चाल से चल रही हों तो जब वे बराबर से गुजरेगी तो 80 मील की चाल का आभास होगा। जब कभी आमने सामने से आती हुई रेल गाड़ियां बराबर से गुजरती हैं तो दूना वेग मालूम पड़ता है, यद्यपि ये दोनों ही अपनी अपनी साधारण चाल से चल रही होती हैं। अपनी पृथ्वी जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है वही गति और दिशा अन्य ग्रह नक्षत्रों की रही होती तो आकाश पूर्णतया स्थिर दीखता। सूर्य तारे कभी न उगते न चलते न डूबते। जो जहां हैं वहीं सदा बना रहता। तब पूर्ण स्थिरता की अनुभूति होते हुये भी सब की गतिशीलता यथावत् बनी रहती।
गति सापेक्ष है। अन्तर कितनी ही तरह निकाला जा सकता है। सौ में से नब्बे निकालने पर दस बचते हैं। तीस में से बीस निकालने पर भी—पचास में से चालीस निकालने पर भी दस ही बचेंगे। अन्तर एक ही निकले इसके लिये अनेकों अंकों का अनेक प्रकार से उपयोग हो सकता है। इतनी भिन्नता रहने पर भी परिणाम में अन्तर न पड़ेगा। एक हजार का जोड़ निकालना हो तो कितने ही अंकों का कितनी ही प्रकार से वही जोड़ बन सकता है। गति मापने के बारे में भी यही बात है। भूतकाल के खगोल वेत्ता सूर्य को स्थिर मान कर यह गणित करते हैं। चन्द्र-ग्रहण, सूर्य ग्रहण सौर मण्डल के ग्रह-उपग्रहों का उदय-अस्त दिन मान, रात्रि मान आदि इसी आधार पर निकाला जाता रहा है। फिर भी वह बिलकुल सही बैठता रहा है। यद्यपि सूर्य को स्थिर मानकर चलने की मान्यता सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या आधार भी जब सत्य परिणाम प्रस्तुतः करते हैं तो फिर सत्य असत्य का भेद किस प्रकार किया जाय, यह सोचने पर बुद्धि थककर बैठ जाती है।
दिशा का निर्धारण भी लोक व्यवहार में आवश्यक है। इसके बिना भूगोल नक्शा, यातायात की कोई व्यवस्था ही न बनेगी। रेखा गणित में आड़ी, सीधी, तिरछी रेखाओं को ही आधार माना गया है। दिशा ज्ञान के बिना वायुयान और जलयानों के लिये निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकना ही सम्भव न होगा। पूर्व, पश्चिम आदि आठ और दो ऊपर नीचे की दशों दिशाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आधार हैं, पर ‘नितान्त सत्य’ का आश्रय लेने पर यह दिशा मान्यता भी लड़खड़ा कर भूमिसात् हो जाती है।
एक लम्बी नाली लगातार खोदते चले जायें तो प्रतीत होगा कि वह सीधी समतल जा रही है, पर वस्तुतः यह गोलाई में ही खुद रही है और वह क्रम चलता रहने पर खुदाई उसी स्थान पर आ पहुंचेगी जहां से वह आरम्भ हुई थी। रबड़ की गेंद पर बिलकुल सीधी रेखा खींचने पर भी वस्तुतः वह गोलाई में ही खिंच रही है, सीधी रेखा खींचने का मतलब उसके दोनों सिरों का अन्तर सदा बना रहना ही होना चाहिये, पर जब वे अन्ततः एक में आ मिलें तो फिर सीधी लकीर कहां हुई? कागज पर जमीन पर, या कहीं भी छोटी बड़ी सीधी लकीर खींची जाय वह कभी भी सीधी नहीं हो सकती। स्वल्प गोलाई अपने नाप साधनों से भले ही पकड़ में न आये, पर वस्तुतः वह गोल ही बन रही होगी। जिस भूमि को हम समतल समझते हैं वस्तुतः वह भी गोल है। समुद्र समतल दीखता है, पर उस पर चलने वाले जहाजों का मस्तूल ही पहले दीखता है इससे प्रतीत होता है कि पानी समतल प्रतीत होते हुये भी पृथ्वी के अनुपात में गोलाई लिये हुये है। जमीन पर खड़े होकर जमीन और आसमान मिलने वाला क्षितिज प्रायः 3 मील पर दिखाई पड़ता है पर यदि दो सौ फुट ऊंचाई पर चढ़ कर देखें तो वह बीस मील दूरी पर मिलता दिखाई देगा। यह बातें पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करती हैं। फिर भी मोटी बुद्धि से उसे गोल देख पाने का कोई प्रत्यक्ष साधन अपने पास नहीं हैं। वह समतल या ऊंची नीची दीखती है गोल नहीं। ऐसी दशा में हमारा दिशाज्ञान भी अविश्वस्त ही ठहरता है। चन्द्रमा हमसे ऊंचा है पर यदि चन्द्रतल पर जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पृथ्वी ऊपर आकाश में उदय होती है। सौर मण्डल से बाहर निकल कर कहीं आकाश में हम जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऊपर नीचे जैसे कोई दिशा नहीं है। दिशाज्ञान सर्वथा अपेक्षाकृत है। दिल्ली, लखनऊ से पश्चिम में बम्बई से पूर्व में, मद्रास से उत्तर में और हरिद्वार से दक्षिण में है। दिल्ली किस दिशा में है यह कहना किसी की तुलना अपेक्षा से ही सम्भव हो सकता है वस्तुतः वह दिशा विहीन है। समय की इकाई लोक व्यवहार में एक तथ्य है। घण्टा मिनट के सहारे ही दफ्तरों का खुलना बन्द होना रेलगाड़ियों का चलना रुकना—सम्भव होता है। अपनी सारी दिनचर्या समय के आधार पर ही बनती है। पर समय की मान्यता भी असंदिग्ध नहीं है। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय वही नहीं होता जो हम देखते या जानते हैं। जब हमें सूर्य उदय होते दीखता है उससे प्रायः 8।। मिनट पहले ही उग चुका होता है। उसकी किरणें पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है। अस्त होता जब दीखता है, उससे 8।। मिनट पूर्व ही वह डूब चुका होता है। आकाश में कितने ही तारे ऐसे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व अस्त हो चुके पर वे अभी तक हमें चमकते दीखते हैं। यह भ्रम इसलिये रहता है कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जब वे वस्तुतः अस्त हुये हैं उसकी जानकारी अब कहीं इतनी लम्बी अवधि के पश्चात हमें मिल रही है। सौर मण्डल के अपने ग्रहों के बारे में भी यही बात है, वे पंचांगों में लिखे समय से बहुत पहले या बाद में उदय तथा अस्त होते हैं।
जो तारा हमें सीध में दीखता है आवश्यक नहीं कि वह उसी स्थिति में है। प्रकाश की गति सर्वथा सीधी नहीं है। प्रकाश भी एक पदार्थ है और उसकी भी तोल है। एक मिनट में एक वर्ग मील जमीन पर सूर्य का जितना प्रकाश गिरता है उसका वजन प्रायः एक ओंस होता है। पदार्थ पर आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तारों का प्रकाश सौर मण्डल में प्रवेश करता है तो सूर्य तथा अन्य ग्रहों के आकर्षण के प्रभाव से लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा तिरछा होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। पर हमारी आंखें उसे सीधी धारा में आता हुआ ही अनुभव करती हैं। हो सकता है कि कोई तारा सूर्य या किसी अन्य ग्रह की ओट में छिपा बैठा हो पर उसका प्रकाश हमें आंखों की सीध में दीख रहा हो। इसी प्रकार ठीक सिर के ऊपर चमकने वाला तार वस्तुतः उस स्थान से बहुत नीचा या तिरछा भी हो सकता है। इस प्रकाश दिशा ही नहीं समय सम्बन्धी मान्यताएं भी निर्भ्रान्त नहीं हैं।
दार्शनिक विवेचनाओं से देश, काल का उल्लेख होता रहता है। उसे कोई मुल्क या घण्टा मिनट वाला समय नहीं समझ लेना चाहिये। यह पारिभाषिक शब्द है। वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई मोटाई को ‘देश’ कहा जाता है और उनके परिवर्तन को ‘काल’। आमतौर से वस्तुएं देश की अर्थात् लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर ही देखी जाती है जब कि उनकी व्याख्या विवेचना करते हुये काल का चौथा ‘आयाम’ भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। किन्तु गतियां और दिशाएं अनिश्चित भी हैं और भ्रामक भी। काल तो उन्हीं पर आश्रित है यदि आधार ही गड़बड़ा रहा है तो काल का परिमाण कैसे निश्चित हो। अस्तु वस्तुओं को तीन आयाम की अपेक्षा चार आयाम वाली भी कहा जाय तो भी बात बनेगी नहीं। वस्तुएं क्या हैं? उनका रूप, गुण, कर्म स्वभाव क्या है? यह कहते नहीं बनता क्योंकि उनके परमाणु जिस द्रुतगति से भ्रमण शील रहते हैं उस अस्थिरता को देखते हुये एक क्षण की गई व्याख्या दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जायगी।
कौन बड़ा कौन छोटा इसका निश्चय भी निःसंकोच नहीं किया जा सकता है। पांच फुट की लकड़ी छह फुट वाली की तुलना में छोटी है और चार फुट वाली की तुलना में बड़ी। एक फुट मोटाई वाले तने की तुलना में दो फुट वाला मोटा ‘अधिक’ है और दो फुट वाले की तुलना में एक फुट वाला पतला। वह वस्तुतः मोटा है या पतला ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तुलना बदलते ही यह छोटा और बड़ा होता—पतला और मोटा होता सहज ही बदल जायेगा।
कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन सुखी है कौन दुःखी, कौन सन्त है, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी, कौन सदाचारी है कौन दुराचारी, इसका निर्णय अनायास ही कर सकना असम्भव है। इस प्रकार का निर्धारण करने से पूर्व यह देखना होगा कि किस की तुलना में निर्णय किया जाय। नितान्त निर्धन की तुलना में वह धनी है जिसके पास पेट भरने के साधन हैं। किन्तु लक्षाधीश की तुलना में वह निर्धन ही है। जिसे दस कष्ट हैं उसकी तुलना में तीन कष्ट वाला सुखी है, पर एक कष्ट वाले की तुलना में वह भी दुःखी है। वस्तुतः कौन सुखी और कौन दुःखी हैं यह नहीं कहा जा सकता। डाकू की तुलना में चोर सहृदय है किन्तु उठाईगीरे की तुलना में वह भी अधिक दुष्ट है। एक सामान्य नागरिक की तुलना में उठाईगीरा भी दुष्ट है, जबकि वह सामान्य नागरिक भी सन्त की तुलना में पिछड़ा हुआ और गया-गुजरा है। सन्त भी किसी महा सन्त आत्मत्यागी शहीद की तुलना में हलका बैठेगा।
अपेक्षा से ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं तुलना ही एक मोटी कसौटी हमारे पास है जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिनके बारे में वह निर्धारण किया गया है वे वस्तुतः क्या हैं? इसका पता लगाना अपनी ज्ञानेन्द्रियों के लिये जिनमें मस्तिष्क भी सम्मिलित है, अति कठिन है। क्योंकि वे सभी अपूर्ण और सीमित हैं। कई अर्थों में तो उन्हें भ्रान्त भी कहा जा सकता है। सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरें चलती-फिरती दिखाई देती हैं वस्तुतः वे स्थिर होती हैं, उनके बदलने का क्रम ही इतना तेज होता है कि आंखें उसे ठीक तरह पकड़ नहीं पातीं और आकृतियों को ही हाथ-पैर हिलाती, बोलती, गाती समझ बैठती हैं।
अक्सर हमारी अनुभूतियां वस्तुस्थिति से सर्वथा उलटी होती हैं। इन्द्रियां अपूर्ण ही नहीं कई बार तो वे भ्रामक सूचनाएं देकर हमें ठगती भी हैं। उनके ऊपर निर्भर रहकर—प्रत्यक्षवाद को आधार मानकर शाश्वत सत्य को प्राप्त करना तो दूर समझ सकना भी सम्भव नहीं होता।
उदाहरण के लिये प्रकाश को ही लें। प्रकाश क्या है? उसे विद्युत चुम्बकीय लहरों का बवंडर ही कहा जा सकता है। वह कितना मन्द या तीव्र है यह तो उसकी मात्रा पर निर्भर है, पर उसकी चाल सदा एक-सी रहती है। एक सैकिण्ड में वह एक लाख छियासी हजार मील की गति से दौड़ते रहने वाला पदार्थ है। प्रकाश किरणों में सात रंग होते हैं! इन्हीं के सम्मिश्रण से हलके भारी अनेकानेक रंगों का सृजन होता है।
कोई रंग नहीं दुनिया में
यह बात कहने, सुनने और जानने, मानने में बड़ी विचित्र लगेगी कि संसार के किसी पदार्थ में कोई रंग नहीं है। हर वस्तु रंग रहित है। किन्तु यह विशेषता अवश्य है कि प्रकाश की किरणों में जो रंग है उनमें से किसी को स्वीकार करें किसी को लौटा दें। बस इसी कारण हमें विभिन्न वस्तुएं विभिन्न रंगों की दीखती हैं। पदार्थ जिस रंग की किरणों को अपने में सोखता नहीं वे उससे टकराकर वापिस लौटती हैं। वापसी में वे हमारी आंखों से टकराती हैं और हम उस टकराव को पदार्थ का अमुक रंग होने के रूप में अनुभव करते हैं। पौधे वस्तुतः हरे नहीं होते, उनका कोई रंग नहीं, हर पौधा सर्वथा बिना रंग का है, पर उसमें प्रकाश की हरी किरणें सोखने की शक्ति नहीं होती अस्तु वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वापिस लौटते हुये हमारी आंखों को इस भ्रम में डाल जाती हैं कि पौधे हरे होते हैं। हम उसी छलावे को शाश्वत सत्य मानते रहते हैं और प्रसंग आने पर पूरा जोर लगाकर यह सिद्ध करते रहते हैं कि पौधे निश्चित रूप से हरे होते हैं। कोई उससे भिन्न बात कहे तो हंसी उसी की बुद्धि पर आवेगी, भ्रांत और दुराग्रही उसी को कहेंगे। यह जानने और मानने का कोई मोटा आधार दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारी ही आंखें धोखा खा रही हैं—प्रकृति की जादूगरी, कलाबाजी हमें ही छल रही हैं। पेड़ का तो उदाहरण मात्र दिया गया। हर पदार्थ के बारे में हम रंगों के सम्बन्ध में ऐसे ही भ्रम जंजाल में जकड़े हुए हैं। जिन आंखों को प्रामाणिक मानते हैं, जिस मस्तिष्क की विवेचना पर विश्वास करते हैं यदि वही भ्रमग्रस्त होकर हमें झुठलाने लगें तो फिर हमारा ‘प्रत्यक्षवाद’ को तथ्य मानने का आग्रह बेतरह धूल धूसरित हो जाता है। हमारी दृष्टि में काला रंग सबसे गहरा रंग है और सफेद रंग कोई रंग नहीं है। पर यथार्थता इस मान्यता से सर्वथा उलटी है। किसी भी रंग का न दीखना काला रंग है और सातों रंगों सम्मिश्रण सफेद रंग। अंधेरा वस्तुतः ‘कुछ भी नहीं’ कहा जा सकता है जबकि वह घेर-घना छाया दीखता है और उसके कारण कुछ भी सूझ न पड़ने की स्थिति आ जाती है। वैशेषिक दर्शन ने अंधेरे को कोई पदार्थ मानने से इनकार किया है, जबकि दूसरे दार्शनिक उसे एक तत्व मानने का जोर-शोर से प्रतिपादन करते हैं। कालापन सभी प्रकाश किरणों को अपने भीतर सोख लेता है। फलतः हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है और अंधेरे में ठोकर खाते हैं—घनी कालिमा छाई देखते हैं।
किसी भी रंग की किरणें सोख सकने में जो पदार्थ सर्वथा असमर्थ हैं वे ही हमें सफेद दीखते हैं। कारण यह है उनसे टकरा कर तिरस्कृत प्रकाश तरंगें वापस लौटती हैं और उनके सातों रंगों का सम्मिश्रण हमारी आंखों को सफेद रंग के रूप में दीखता है। कैसी विचित्र, कैसी असंगत और कैसी भ्रम जंजाल भरी विडम्बना है यह। जिसे न उगलते बनता है न पीते। न स्वीकार करने को मन होता है अस्वीकार करने का साहस। अपने ही अपूर्ण उपकरणों पर क्षोभ व्यक्त न करते हुये मन मसोस कर बैठना पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धियों को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। हलका, भारी, गहरा, उथला कालापन भी एक पहेली है। अन्धकार कहीं या कभी बहुत गहरा होता है और कहीं या कभी उसमें हलकापन रहता है यह भी उतने अंशों में प्रकाश को सोखने न सोखने की क्षमता पर निर्भर रहता है। काले रंग में प्रकाश का सारा अंश सोख लेने की क्षमता का एक प्रमाण यह है कि वह धूप में अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी गरम होता है।
अब एक नया प्रश्न उभरता है कि प्रकाश किरणों में रंग कहां से आता है? इस स्थल पर उत्तर और भी विचित्र बन जाता है। प्रकाश लहरों की लम्बाई का अन्तर ही रंगों के रूप में दीखता है। वस्तुतः रंग नाम की कोई चीज समस्त विश्व में कहीं कुछ है ही नहीं। उसका अस्तित्व सर्वथा भ्रामक है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही प्रकाश हैं। इन तरंगों की लम्बाई अलग-अलग होती है। अस्तु उनका अनुभव हमारा मस्तिष्क भिन्न-भिन्न अनुभूतियों के साथ करता है। यह अनुभूति भिन्नता ही रंगों के रूप में विदित होती है। सात रंग तथा उनसे मिल-जुलकर बनने वाले अनेकानेक रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रकाश तरंगों की लम्बाई का मस्तिष्कीय अनुभूति के रूप में ही किया जा सकता है। रंगों की अपनी तात्विक सत्ता कुछ भी नहीं है।
आश्चर्य का अन्त इतने से ही नहीं हो जाता। रंगों की दुनिया बहुत बड़ी है उसे मेले में हमारी जान-पहचान बहुत थोड़ी-सी है। बाकी तो सब कुछ अनदेखा ही पड़ा है। लाल रंग की प्रकाश तरंगें एक इंच जगह में तेतीस हजार होती हैं जबकि कासनी रंग की सोलह हजार। इन्फ्रारेड तरंगें एक इंच में मात्र 80 ही होती हैं। इसके विपरीत रेडियो तरंगों की लम्बाई बीस मील से लेकर दो हजार मील तक पाई जाती है। यह अधिक लम्बाई की बात हुई। अब छोटाई की बात देखी जाय परा कासनी किरण एक इंच में बीस लाख तक होती हैं। एक्सरे किरणें एक इंच में पांच करोड़ से एक अरब तक पाई जाती हैं। गामा तरंगें एक इंच में 220 अरब। इतने पर भी इन सब की चाल एक जैसी है अर्थात् सैकिण्ड में वही एक लाख छियासी हजार मील।
अगर हम विदित प्रकाश किरणों को यन्त्रों की अपेक्षा खुली आंखों से देख सकने में समर्थ हो सके होते तो जिस प्रकाश एक सात रंगों का सप्तक हमें दीखता है उससे अतिरिक्त अन्यान्य ऐसे रंगों के जिनकी आज तो कल्पना कर सकना भी अपने लिए कठिन है 67 सप्तक और दीखते। 67×7=469 रंगों के सम्मिश्रण से कितने अधिक रंग बन जाते इसका अनुमान इसी से लगाया जाता है कि विज्ञान सात रंगों से ही हजारों प्रकार के हलके भारी रंग बने हुए दीखते हैं।
प्रातःकाल का अरुणोदय और लाल रंग का सूर्य निकलना इस रंग भ्रम जंजाल की एक झलक है। सूर्य वस्तुतः सफेद ही होता है, पर सवेरे वह सिर पर नहीं पूर्व में तिरछी स्थिति में होता है। इसलिए उसकी किरणों को बहुत लम्बा वायुमंडल पार करना पड़ता है। इस मार्ग में बहुत अधिक धूलि कण आड़े आते हैं। वे कण लाल रंग नहीं सोख पाते अस्तु वे किरणें हम तक चली आती हैं और सवेरे का उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई पड़ता है।
आंखें कितना अधिक धोखा खाती हैं और मस्तिष्क कितनी आसानी से बहक जाता है इसका एक उदाहरण रंगों की दुनिया में पहला पैर रखते ही विदित हो जाता है। अन्य विषयों में भी हमारी भ्रान्ति का ठिकाना नहीं। जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और लक्ष्य एक प्रकार से पूरी तरह विस्मृत कर दिया है और जड़ पदार्थों पर अपनी ही मान्यता को बखेर कर उन्हें प्रिय-अप्रिय के रूप में देखने की स्थिति को संसार से मिलने वाले सुख-दुख मान लिया है। आत्म-ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि यदि मिल सके तो पता लगेगा कि हम अज्ञान, माया और भ्रम के जिस जंजाल में फंसे हुए हैं उनसे निकले बिना सत्य के दर्शन नहीं हो सकते और सत्य के बिना सुख नहीं मिल सकता।
वेदान्त दर्शन संसार को माया बताता है और संसार को स्वप्न कहता है इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ दीखता है उसका अस्तित्व ही नहीं अथवा जो सामने है वह झूठ है। वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति में वे सत्य भी हैं। यदि ऐसा न होता तो कर्म फल क्यों मिलते? पुण्य और तप तितीक्षा करने की क्या आवश्यकता होती। कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या अन्त होता? धर्मकृत्यों की क्या उपयोगिता रह जाती? और पाप कर्मों से डरने बचने की क्या आवश्यकता रहती?
माया का अर्थ वेदान्त ने इस अर्थ में किया है जिसमें जो भाषित होता हो वह तत्वतः यथार्थ न हो। जगत को इसी स्थिति में—इसी स्तर का माना गया है। वह जैसा कुछ प्रतीत होता है, क्या वह वैसा ही है? इस प्रश्न पर जब गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि संसार में जो कुछ हम इन्द्रियों द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं वह यथार्थ में वैसा ही नहीं होता। इन्द्रिय छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क को होने वाली अनुभूतियों का नाम ही जानकारी तभी सत्य हो सकती है जब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को सही रूप में इन्द्रियां समझ सकें। यदि वे धोखा खाने लगें तो मस्तिष्क गलत अनुभव करेगा और वस्तुस्थिति उलटी दिखाई पड़ने लगेगी।
नशा पी लेने पर मस्तिष्क और इन्द्रियों का संबंध लड़खड़ा जाता है, फलस्वरूप कुछ का कुछ अनुभव होता है शराब के नशे में धुत्त व्यक्ति जैसा कुछ सोचता, समझता, देखता अनुभव करता है वह यथार्थता से बहुत भिन्न होता है। और भी ऊंचे नशे इस उन्मत्तता की स्थिति को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। डी. एलस्केस. ए. सरीखे नवीन नशे तो इतने तीव्र हैं कि उनके सेवन के उपरान्त ऐसे विचित्र अनुभव मस्तिष्क को होते हैं जिनकी यथार्थता के साथ कोई संगति नहीं होती।
साधारणतया दैनिक जीवन में भी अधिकांश अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें यथार्थ नहीं कहा जा सकता। सिनेमा के पर्दे पर जो दीखता है सही कहां है? एक के बाद एक आने वाली अलग-अलग तस्वीरें इतनी तेजी से घूमती हैं कि उस परिवर्तन को आंखें ठीक तरह समझ नहीं पातीं और ऐसा भ्रम होता है मानो फिल्म में पात्र चल फिर रहे हैं। लाउडस्पीकर से शब्द अलग अन्यत्र निकलते हैं और पर्दे पर तस्वीर के होठ अलग चलते हैं पर दर्शकों को ऐसा ही आभास होता रहता है मानो अभिनेताओं के मुख से ही वार्तालाप एवं संगीत निकल रहा है। प्रकाश की विरलता और सघनता भर पर्दे पर उतरती है पर उसी से पात्रों एवं दृश्यों का स्वरूप बन जाता है और मस्तिष्क ऐसा अनुभव करता है मानो यथार्थ ही वह घटना क्रम घटित हो रहा है।
सिनेमा के दृश्य क्रम को देखकर आने वाला यह नहीं अनुभव करता कि उसे यांत्रिक जाल जंजाल में ढाई तीन घंटे उलझा रहना पड़ा है। उसे जो दुखद-सुखद रोचक भयानक अनुभूतियां उतने समय होती रही हैं वे सर्वथा भ्रान्त थीं। सिनेमा हाल में कोई घटना क्रम नहीं घटा। कोई प्रभावोत्पादक परिस्थिति नहीं बनी केवल प्रकाश यन्त्र या ध्वनि यन्त्र अपने-अपने ढंग की कुछ हरकतें भी करते रहे। इतने भर से दर्शक अपने सामने अति महत्वपूर्ण घटना क्रम उपस्थित होते का आभास करता रहा, इतना ही नहीं उससे हर्षातिरेक एवं अश्रुपात जैसी भाव भरी मनःस्थिति में भी बना रहा। इस इन्द्रिय भ्रम को माया कहा जाता है। मोटी दृष्टि से यह माया सत्य है। यदि सत्य न होती तो फिल्म उद्योग, सिनेमा हाल, उसमें युक्त हुए यन्त्र, दर्शकों की भीड़ उनकी अनुभूति आदि का क्या महत्व रह जाता? थोड़ी विवेचनात्मक गहराई से देखा जाय तो यह यन्त्रों की कुशलता और वस्तुस्थिति को समझ न सकने को नेत्र असमर्थता के आधार पर इस फिल्म दर्शन को मायाचार भी कह सकते हैं। दोनों ही तथ्य अपने अपने ढंग से सही हैं। संसार चूंकि हमारे सामने खड़ा है, उसके घटना क्रम को प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए वह सही है किन्तु गहराई में प्रवेश करने पर वे दैनिक अनुभूतियां नितान्त भ्रामक सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन्हें भ्रम, स्वप्न या माया कहना भी अत्युक्ति नहीं है।
स्पष्ट है सभी दृश्य पदार्थ एक विशेष प्रकार के परमाणुओं का एक विशेष प्रकार का संयोग मात्र हैं। प्रत्येक परमाणु अत्यन्त तीव्र गति से गतिशील है। इस प्रकार हर पदार्थ अपनी मूल स्थिति में आश्चर्यजनक तीव्र गति से हरकत कर रहा है। पर खुली आंखें यह सब कुछ देख नहीं पातीं और वस्तुएं सामने जड़वत् स्थिर खड़ी मालूम पड़ती है। ऐसा ही अपनी पृथ्वी के बारे में भी होता है। भूमण्डल अत्यन्त तीव्र गति से (1) अपनी धुरी पर (2) सूर्य की परिक्रमा के लिए अपनी कक्षा पर (3) सौर मंडल सहित महासूर्य की परिक्रमा के पथ पर (4) घूमता हुआ लट्टू जिस तरह इधर उधर लहकता रहता है उस तरह लहकते रहने के क्रम पर (5) ब्रह्माण्ड के फलते फूलते जाने की प्रक्रिया के कारण अपने यथार्थ आकाश स्थान को छोड़ कर फैलता स्थान पकड़ते जाने की व्यवस्था पर—निरन्तर एक साथ पांच प्रकार की चालें चलती रहती हैं। इस उद्धत नृत्य को हम तनिक भी अनुभव नहीं करते और देखते हैं कि जन्म से लेकर मरण काल तक धरती अपने स्थान पर जड़वत् जहां की तहां पड़ी रही है। आंखों के द्वारा मस्तिष्क को इस सम्बन्ध में जो जानकारी दी जाती है और जैसी कुछ मान्यता आमतौर से बनी रहती है उसका विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होगा कि हम भ्रम अज्ञान की स्थिति में पड़े रहते हैं और कुछ का कुछ अनुभव करते रहते हैं, यह माया ग्रस्त स्थिति कही जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी।
जल में सूर्य चन्द्र के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं और लगता है कि पानी में प्रकाश पिण्ड जगमगा रहे हैं। हल लहर पर प्रतिबिम्ब पड़ने से हर लहर पर एक चन्द्रमा नाचता थिरकता मालूम पड़ता है। रेल में बैठने वाले देखते हैं कि वे अपने स्थान पर स्थिर बैठे हैं केवल बाहर तार के खंभे और पेड़ आदि भार रहे हैं। क्या यह अनुभूतियां सत्य हैं। रात्रि को स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ने वाला घटना क्रम यथार्थ मालूम पड़ता है। देखते समय दुख-सुख भी होता है। यदि यथार्थ में संदेह होता तो कई बार मुख से कुछ शब्द निकल पड़ना—स्वप्नदोष आदि हो जाने की बात क्यों होती? जागने पर स्पष्ट हो जाता है कि जो अपना देखा गया था उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं था। केवल कल्पनाओं की उड़ान को निद्रित मस्तिष्क ने यथार्थता अनुभव कर लिया। उतने समय की मूर्छित मनःस्थिति अपने को भ्रम जंजाल में फंसाये रह कर बेसिर पैर की उड़ानों में उड़ाती रही।
अंधेरे में झाड़ी भूत जैसी लगती है—रस्सी का टुकड़ा सांप प्रतीत होता है, मरीचिकाएं थल में जल का और जल में थल का भान कराती हैं। यथार्थता से सर्वथा भिन्न अनुभूतियों का होना कोई अनहोनी बात नहीं है। आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने वाले वायुयान छोटे पक्षी जैसे लगते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुने बड़े और अपने सूर्य से हजारों गुने अधिक चमकदार तारागण नन्हे से दीपक की तरह टिमटिमाते दीखते हैं। क्या यह सारे दृश्य यथार्थ में वैसे ही हैं जैसे कि आंखें हमें अनुभव कराती हैं? आंखों की तरह ही अन्य इन्द्रियों की बात है। वे एक सीमा तक ही वस्तुस्थिति का ज्ञान कराती हैं और जो बताती जताती हैं उसमें से भी अधिकांश भ्रान्त होता है। बुखार आने पर गर्मी की ऋतु में शीत का और शीत में गर्मी का अनुभव होता है। मुंह का जायका खराब होने पर हर चीज कड़वी लगती है। जुकाम हो जाने पर चारों ओर बदबू का अनुभव होता है। पीलिया रोग होने पर आंखें पीली हो जाती हैं और हर चीज पीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्या यह अनुभूतियां सही होती हैं?
जिस वस्तु का जैसा स्वाद प्रतीत होता है वह वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य को जो नीम के पत्ते कडुए लगते हैं, वे ऊंट को भी वैसे ही क्यों न लगते, वह उन्हें रुचि पूर्वक स्वादिष्ट पदार्थों की तरह क्यों खाता? खाद्य पदार्थों का स्वाद हर प्राणी की जिह्वा से निकलते रहने वाला अलग अलग स्तर के रसों तथा मुख के ज्ञान तन्तुओं की बनावट पर निर्भर है। भोजन मुंह में गया—वहां के रसों का सम्मिश्रण हुआ और उस मिलाप की जैसी कुछ प्रतिक्रिया मस्तिष्क पर हुई उसी का नाम स्वाद की अनुभूति है। खाद्य पदार्थ की वास्तविक रासायनिक स्थिति इस स्वाद अनुभूति से सर्वथा भिन्न है। जो कुछ चखने पर अनुभव होता है वह यथार्थता नहीं है।
शरीर विज्ञानी जानते हैं कि काया का निर्माण अरबों खरबों कोशिकाओं के सम्मिलन से हुआ है। उनमें से प्रतिक्षण लाखों मरती हैं और नई उपजती हैं। यह क्रम बराबर चलता रहता है और थोड़े ही दिनों में, कुछ समय पूर्व वाली समस्त कोशिकाएं मर जाती हैं और उनका स्थान नई ग्रहण कर लेती हैं। इस तरह एक प्रकार से शरीर का बार-बार काया कल्प होता रहता है। पुरानी वस्तु एक भी नहीं रहती उनका स्थान नये जीव कोष ग्रहण कर लेते हैं। देह के भीतर एक प्रकार श्मशान जलता रहता है और प्रसूति ग्रह में प्रजनन की धूम मची रहती है। इतनी बड़ी हलचल का हमें तनिक भी बोध नहीं होता और लगता है देह जैसी की तैसी रहती है। जिन इन्द्रियों के सहारे हम अपना काम चलाते हैं उनमें इतना भी दम नहीं होता कि बाहरी वस्तुस्थिति बनाना तो दूर अपने भीतर की इतनी महत्वपूर्ण हलचलों का तो आभास दे सकें। ऐसी इन्द्रियों के आधार पर यथार्थ जानकारी का दावा कैसे किया जाय? जिस मस्तिष्क को अपने कार्यक्षेत्र-शरीर के भीतर होने वाले रोगों में क्या स्थिति बनी हुई है, इतना तक ज्ञान नहीं है और घर की बात को बाहर वालों से पूछना पड़ता है वैद्य डाक्टरों का दरवाजा खट-खटाना पड़ता है, उस मस्तिष्क पर यह भरोसा कैसे किया जाय कि वह इस ज्ञान का वस्तुस्थिति में हमें सही रूप में अवगत करा देगा।
ज्ञान जीवन का प्राण है। पर वह होना यथार्थ स्तर का चाहिए। यदि कुछ का कुछ समझा जाय, उलटा देखा और जाना जाय, भ्रम विपर्यय हमारी जानकारियों का आधार बन जाय तो समझना चाहिए यह ज्ञान प्रतीत होने वाली चेतना वस्तुतः अज्ञान ही है। उसमें जकड़े रहने पर हमें विविध विधि त्रास ही उठाने पड़ेंगे, पग-पग पर ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसी स्थिति को माया कहते हैं। माया कोई बाहरी संकट नहीं, मात्र भीतरी भ्रान्ति भरी मनःस्थिति ही है, यदि उसे सुधार लिया जाय, तो समझना चाहिए माया के बन्धनों से मुक्ति मिल गई यह मुक्ति वस्तुतः हर किसी के करतलगत है।