युग की माँग प्रतिभा परिष्कार-भाग २ 
प्रतिभा बनाम तेजस्विता बनाम तपश्चर्या
Read Scan Version
मनुष्य अन्य जीवधारियों से भिन्न है। उसकी शारीरिक संरचना इतनी अद्भुत है
कि वह कलाकौशल के क्षेत्र में न जाने क्या- क्या चमत्कार दिखा सकता है।
उसका बुद्धि संस्थान इतना अद्भुत है कि सुविधा- साधनों की बात ही क्या, वह
उसके बलबूते वैज्ञानिक के रूप में प्रकृति का रहस्योद्घाटन और प्राणि- जगत
का भाग्य निर्माता होने तक का दावा कर रहा है। विद्या बुद्धि से संबंधित
अनेकानेक तत्त्वदर्शन उसने विनिर्मित किए हैं। शासन और समाज की संरचना उसी
की सूझबूझ का प्रतिफल है। साहित्य का अक्षय भंडार उसी का सृजा हुआ है। उसी
ने देवी- देवताओं की सृष्टी की है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि ईश्वर
ने भले ही सृष्टि को बनाया हो, पर ईश्वर जिस भी रूप में आज लोकमानस में
स्थान पा सका है, वह मनुष्य की ही प्रतिष्ठापना है। इस दृष्टि से तो वह
स्रष्टा का भी स्रष्टा हुआ न? कैसा अद्भुत है यह गले न उतरने वाला सत्य और
तथ्य। मनुष्य सचमुच महान् है। दार्शनिकों ने उसे भटका हुआ देवता कहा है।
शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में और कुछ नहीं है।
बात बहुत हद तक सही भी मालूम पड़ती है, क्योंकि अवतारों से लेकर महामानवों तक का इतिहास एक ही बात बताता है कि मनुष्य अपने आप को समझ और विकसित कर सके तो वह उस स्तर को तक पहुँच सकता है, जिसका प्रतिपादन, वेदांत दर्शन की शिवोऽहम्, सच्चिदानंदोऽहम् अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि आदि उक्तियों के माध्यम से, उसे ईश्वर सिद्ध करता है। ईश्वर का राजकुमार या प्रतिनिधि होने का दावा तो अनेकों मूर्द्धन्यों ने अनेक बार किया है। ईसा को ईश्वर का पुत्र होने की मान्यता मिली है।
यह पृथ्वी अनादिकाल से ऊबड़- खाबड़ खाई- खड्डों से भरी हुई अनगढ़ जीव- जन्तुओं की क्रीड़ास्थली रही होगी। उसे आज की स्थिति में लाने और स्वर्गादपि गरीयसी बनाने में मनुष्य की कलाकारिता की ही प्रधान भूमिका रही है। वनमानुष या नर- वानर की आदिम स्थिति से ऊपर उठकर उसने अपने को क्या- से बना लिया, इसे देखकर हैरत में रह जाना पड़ता है। प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियाँ कभी स्रोतों को हस्तगत कर लेने से लेकर अंतरिक्ष पर साम्राज्य स्थापित करने तक की ठानी है। मनुष्य सचमुच वह है, जो कुछ इस ब्रह्मांड में महान् से महानतम हो सकता है।
आश्चर्य इस बात का है कि उसे भटकाव ने इस बुरी तरह से जकड़ा कि वह अपने अस्तित्व, महत्त्व एवं स्तर के संबंध में इतना अधिक दिग्भ्रांत हो गया है कि उसे भटकाव की चरम सीमा कहा जा सकता है।
भटकाव का पहला सोपान वहाँ से आरंभ होता है, जहाँ मनुष्य अपनी, सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता के संबंध में लगभग पूरी तरह विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। अपनी आकृति- प्रकृति की भिन्नता को तो देखता है, पर यह नहीं सोच पाता कि वह पशुस्तर के प्राणियों से चेतना के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट है। प्राणी पेट भरने और प्रजनन के कौतुक का रसास्वादन करने के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें न मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा होती है और न वर्जनाओं से बचने की आस्था। बंधनों, उत्तेजनाओं और अवरोधों से बाधित होकर ही वे अनुचित को अपनाने से रुक पाते हैं। स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में उन्हें मर्यादा पालन में कोई उत्साह नहीं रहता। आवश्यकता और मनमरजी ही उनकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मनुष्य की भावना और धारणा भी ऐसी हो, तो उसे नर- पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिनने लोभ, मोह और अहंकार की लिप्सा- लालसा को ही अपना लक्ष्य मान लिया है, वे उचित- अनुचित का अंतर किस प्रकार कर सकेंगे? संकीर्ण स्वार्थपरता के भव- बंधनों से छुटकारा पा सकना उनसे कैसे बन पड़ेगा?
बात बहुत हद तक सही भी मालूम पड़ती है, क्योंकि अवतारों से लेकर महामानवों तक का इतिहास एक ही बात बताता है कि मनुष्य अपने आप को समझ और विकसित कर सके तो वह उस स्तर को तक पहुँच सकता है, जिसका प्रतिपादन, वेदांत दर्शन की शिवोऽहम्, सच्चिदानंदोऽहम् अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि आदि उक्तियों के माध्यम से, उसे ईश्वर सिद्ध करता है। ईश्वर का राजकुमार या प्रतिनिधि होने का दावा तो अनेकों मूर्द्धन्यों ने अनेक बार किया है। ईसा को ईश्वर का पुत्र होने की मान्यता मिली है।
यह पृथ्वी अनादिकाल से ऊबड़- खाबड़ खाई- खड्डों से भरी हुई अनगढ़ जीव- जन्तुओं की क्रीड़ास्थली रही होगी। उसे आज की स्थिति में लाने और स्वर्गादपि गरीयसी बनाने में मनुष्य की कलाकारिता की ही प्रधान भूमिका रही है। वनमानुष या नर- वानर की आदिम स्थिति से ऊपर उठकर उसने अपने को क्या- से बना लिया, इसे देखकर हैरत में रह जाना पड़ता है। प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियाँ कभी स्रोतों को हस्तगत कर लेने से लेकर अंतरिक्ष पर साम्राज्य स्थापित करने तक की ठानी है। मनुष्य सचमुच वह है, जो कुछ इस ब्रह्मांड में महान् से महानतम हो सकता है।
आश्चर्य इस बात का है कि उसे भटकाव ने इस बुरी तरह से जकड़ा कि वह अपने अस्तित्व, महत्त्व एवं स्तर के संबंध में इतना अधिक दिग्भ्रांत हो गया है कि उसे भटकाव की चरम सीमा कहा जा सकता है।
भटकाव का पहला सोपान वहाँ से आरंभ होता है, जहाँ मनुष्य अपनी, सत्ता, महिमा, गरिमा और क्षमता के संबंध में लगभग पूरी तरह विस्मृति की खुमारी में चला जाता है। अपनी आकृति- प्रकृति की भिन्नता को तो देखता है, पर यह नहीं सोच पाता कि वह पशुस्तर के प्राणियों से चेतना के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट है। प्राणी पेट भरने और प्रजनन के कौतुक का रसास्वादन करने के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें न मर्यादाओं के प्रति श्रद्धा होती है और न वर्जनाओं से बचने की आस्था। बंधनों, उत्तेजनाओं और अवरोधों से बाधित होकर ही वे अनुचित को अपनाने से रुक पाते हैं। स्वच्छंदता और क्षमता रहने की स्थिति में उन्हें मर्यादा पालन में कोई उत्साह नहीं रहता। आवश्यकता और मनमरजी ही उनकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मनुष्य की भावना और धारणा भी ऐसी हो, तो उसे नर- पशु से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिनने लोभ, मोह और अहंकार की लिप्सा- लालसा को ही अपना लक्ष्य मान लिया है, वे उचित- अनुचित का अंतर किस प्रकार कर सकेंगे? संकीर्ण स्वार्थपरता के भव- बंधनों से छुटकारा पा सकना उनसे कैसे बन पड़ेगा?
जिन्हें संपन्नता की तृष्णा और बड़े कहलाने की
महत्त्वाकांक्षाएँ जकड़े रहती हैं, उनके लिए विचारशीलता के स्वच्छंद आकाश
में पंख फड़फड़ाना कैसे संभव है? आम आदमी साधनों और क्षमताओं की दृष्टि से
कैसा ही क्यों न दीख पड़े, पर उसे आदर्शों की उमंगें प्रभावित ही नहीं
करतीं। उत्कृष्टता की गरिमा अपनाने के लिए उमंगें ही नहीं उठतीं। पुण्य और
परमार्थ का प्रसंग तो एक प्रकार से छूट ही जाता है, जिसके लिए स्रष्टा ने
मानवी उत्कृष्टता का, लगभग देवोपम स्तर का सृजन विशेष रूप से किया है। उसके
पूरी तरह छूट जाने के उपरांत व्यक्ति क्षुद्र कृमि- कीटकों की गई−गुजरी
श्रेणी में ही गिने जाने योग्य रह जाता है, भले ही वह पदाधिकारी, पदवीधारी,
संपन्न, कुशल एवं विभूतिवान् ही क्यों न समझा जाता हो? यह सुविधाएँ मात्र
शारीरिक विलासिता, सज्जा अथवा इठलाने भर के काम आती हैं। अंतःचेतना को इनकी
बहुलता से न तो संतोष होता है और न उल्लास मिलता है, जिसके आधार पर वह
अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर सके। यही है वह अभाव जिसके बिना हर घड़ी
उद्विग्नता एवं खीझ छाई रहती है।
धर्मचर्चा तो कई लोग करते और सुनते रहते हैं, पर होता वह सब कुछ खोखला ही है। लोग पूजा- पाठ के कर्मकाण्डों, तीर्थ- पर्यटनों भजन- प्रदर्शन की विडम्बनाओं से मन बहलाते और अपने को धर्मध्वजी मानते देखे गए हैं पर बात वस्तुत: वैसी है नहीं। कर्मकाण्डों का एक मात्र मंतव्य यह है कि चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक शालीनता का समावेश करें। जिन्हें धर्म में वस्तुतः: कुछ रुचि है, उन्हें देवोपम स्तर का जीवनयापन करते देखा जाना चाहिए। उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रामाणिकता एवं प्रखरता से भरे होने चाहिए। अनौचित्य को अपनाकर भी लोग सुविधा- साधनों का संग्रह और चारण- चाटुकारों के माध्यम से मिल सकने वाली प्रशंसा बटोर लेते हैं, पर उनमें न तो यह गहराई होती है न स्थिरता। धुएँ से बने बादल कितने ही घने क्यों न हों, हवा के एक झोंके में जिधर- तिधर बिखर जाते हैं। छलावा पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गँवा बैठता है।
प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंत:सत्ता में भरे पड़े हैं, उन्हें उभरने- प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण आने ही नहीं पाता, जो कषाय- कल्मषों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिए गए हैं। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बाँध दी जाएँ तो अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान् होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में रह ही नहीं जाता।
प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से अंतराल को और दुष्ट आचरण से काय कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। यह तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्त्वाकाँक्षाओं की हथकड़ी- बेड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धनाढ्य बनने में रहती है, ताकि विलासिता के विपुल साधन जुटाए जा सकें, साथ ही अभावग्रस्तों की बिरादरी में अपने को बढ़ा- चढ़ा सिद्ध करने की मूँछें मरोड़ी जा सकें। इतनी छोटी सीमा में जिनका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया हैं, वे उन महान् कार्यों के प्रति उन्मुख ही नहीं हो सकते, जो मानवी गरिमा में चार चाँद लगाते हैं। खूँटे से बँधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहाँ बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित व्यक्ति न तो आदर्शवादिता अपना सकता है और न ऐसा कुछ कर सकता है, जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वेश्याएँ भी अपने को परी जैसी सुंदर दिखाने का भ्रम रचती रहती हैं।
प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य हैं, जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर अड़े होते हैं। इस संदर्भ में स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अंगीकार किया जाए, अन्यथा तृष्णा और वासना की लिप्सा इतनी सघनता के साथ छाई रहेगी कि अपनी सामर्थ्य की तुलना में अकिंचन जितना परमार्थ भी करते न बन पड़ेगा। यह खाइयाँ इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है कि छोटे- से जीवन का समूचा साधन, श्रम, कौशल खपा देने पर भी उन्हें भरा नहीं जा सकता। फिर वह बन ही कैसे पड़े जो उत्कृष्टता के साथ अति सघनतापूर्वक जुड़े हुए प्रतिभा- परिष्कार का पुण्य- प्रयोजन संतोषजनक मात्रा में उपलब्ध करा सके।
लालसा- जन्य महत्त्वाकाँक्षाओं में कटौती किए बिना किसी के पास भी इतना समय, श्रम, साधन बच नहीं सकता, जिसके सहारे आत्मकल्याण और लोक कल्याण की दिशा में कुछ कहने लायक कदम उठ सकें। साधु और ब्राह्मणों को भूसुर की, पृथ्वी के देवता की उपमा दी जाती रही है। वह इसलिए कि उसने संयम, अपरिग्रह, संतोष की राह अपनाई। अपने निजी बड़प्पन में जिनकी जितनी अभिरुचि होगी, वह उतना ही अपने को व्यस्त और अभावग्रस्त अनुभव करेगा। सदा यही कहता रहेगा कि अपनी समस्याओं से ही घिरा हुआ हूँ, जबकि वस्तुत: वास्तविक समस्याएँ मनुष्यों के सामने होती ही कितनी है? फिर यदि उन्हें व्यावहारिक बुद्धि द्वारा समझदारी के साथ सुलझाया जाए, तो इतनी सरलतापूर्वक सुलझ जाती हैं, मानों वे वस्तुतः: थीं ही नहीं। भ्रांतियों के कारण वे बढ़ी या लाद दी गई हैं।
संयम- नियम के कितने ही अनुबंध हैं, जिनमें आहार- विहार की शुद्धि, सज्जनता, सद्भावना, श्रमशीलता, मितव्ययिता, स्वच्छता, सहकारिता, अनुशासन, प्रियता आदि प्रमुख हैं। इनके विपरीत अनेक दोष हैं- असंयम चटोरपन, आलस्य, प्रमाद, निष्ठुरता, स्वच्छंदता, अपव्यय, व्यसन आदि जो प्रगति में बाधक बनते हैं। यह सब देखने- सुनने में बहुत ही दुष्कर प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः: हैं संकीर्ण स्वार्थपरता और स्वेच्छाचार की पैदा की हुई औलाद ही। इनमें से एक- एक को गिनना और रोकथाम करना मेंढक तोलने के समान है। बिस्तर को धूप में डाल देने के उपरांत खटमल और उनके अंडे- बच्चे सभी मर जाते हैं। इसी प्रकार दृष्टिकोण को उदात्त बना लेने के उपरांत अपना स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य तीनों ही सूझ पड़ते हैं। उस प्रकाश के जलते ही उन भूत- पलीतों से छुटकारा मिल जाता है, जो अँधेरे के कारण सामान्य होते हुए भी, डरावने बनकर भयभीत करते और त्रास देते थे।
दृष्टिकोण में जब विशालता का समावेश होता है तो लगता है कि परमार्थ ही परम स्वार्थ है। इसके बराबर लाभ और किसी व्यवसाय में नहीं। इस तथ्य को इतिहास प्रसिद्ध सभी महामानवों से लेकर सामयिक श्रद्धाभाजन व्यक्तियों के ऊपर बरसती हुई सद्भावना को देखकर सहज समझा जा सकता है, कि व्यक्तिगत लाभ की बात सोचने वाले भी यदि दूरदर्शी हों, तो उन्हें परमार्थ प्रयोजनों में अपनी क्षमता लगाने के उपरांत बदले में कई गुना होकर लौटता है। यही नीति महामानवों की रहती है। वे समाज के खेत में पुण्यपरमार्थ के बीज बिखेर देते हैं और उस फसल को अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी काटते व विश्ववसुधा को लाभान्वित करते हैं। यही प्रतिभा का चिह्न है।
प्रतिभा, तेजस्विता को कहते हैं। यह चेहरे की चमक या चतुरता नहीं, वरन् मनोबल पर आधारित ऊर्जा है। गाँधी जी ९२ पौंड वजन और ५ फुट २ इंच के थे। रंग के काले और कुरूप भी, पर उनका तेजस् ऐसा था कि जनसाधारण से लेकर देश के वरिष्ठ मूर्द्धन्यों तक को उनका आदेश शिरोधार्य करते देखा जा सकता था। यहाँ तक कि विशाल साम्राज्य के अधिपति अंग्रेज भी उनसे प्रभावित होकर बिस्तर गोल करके चले ही गए। यह तेजस् निजी और सामूहिक जीवन के हर पक्ष को जगमगाता है। उसे प्रखरता भरी ऊर्जा से जाज्वल्यमान बना देता है।
तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है, जो निजी जीवन में संयम- साधना और सामाजिक जीवन में परमार्थपरायणता के फलस्वरूप उद्भूत होती हैं। संयम अर्थात अनुशासन का, आत्मनियंत्रण कठोरतापूर्वक परिपालन। इसके लिए मनुष्य को तृष्णा, वासना और अहंता के त्रिविध नागपाशों से छूटता पड़ता है। ‘सादा जीवन उच्च विचार’ का ब्राह्मणोचित औसत नागरिक स्तर का जीवनयापन करना पड़ता है। जो इतना कर सके, उन्हीं से परमार्थ सधता है और योगियों में पाई जाने वाली सिद्धियों, शक्तियों और विभूतियों का अंतराल में उद्भव और अखिल अंतरिक्ष से अभिवर्षण होता है। दैवी अनुग्रह या वरदान भी इसी को कहते हैं।
कर्मकाण्डपरक इसके साधना- विधान अनेक हैं, पर सर्वसुलभ प्रक्रिया यही है कि निजी जीवन इतना हलका- फुलका रखा जाए कि उसका निर्वाह न्यूनतम श्रम और समय में ही संभव होता रहे। इसके उपरांत ही श्रम, समय और साधन इतनी मात्रा में बच पाते हैं कि उनके आधार पर परमार्थ में निरत रहकर परब्रह्म के साथ एकात्म होने का रसास्वादन किया जा सके, देवोपम जीवन जीने का आनंद लाभ उठाया जा सके।
किस प्रयोजन के लिए, किस अवसर पर, किस प्रकार, क्या संयम बरता जाय? यह निर्णय- निर्धारण व्यक्ति विशेष की परिस्थिति और मनःस्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। जिसके जीवन का जो पक्ष उद्धत हो चला हो, उसे सरकस के जानवरों की तरह बलचातुर्य प्रयोग करते हुए कलाकौशल दिखा सकने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। शरीर और मन दोनों को ही शालीनता अपनाए रहने के अभ्यस्त करना पड़ता है। संयम योग यही है। जो इतना कर सका, वही पुण्य- परमार्थ अर्जित करने का भी अधिकारी है। उद्धत आचरण वाला व्यक्ति कीचड़- से धोने के प्रयत्न में क्या कुछ सफलता प्राप्त कर सकेगा? शालीनता और परमार्थपरायणता मिलकर ही तपश्चर्या बनती हैं और उन्हीं के आधार पर प्रतिभा की ऊर्जा अपनी प्रचंडता का परिचय देती है।
धर्मचर्चा तो कई लोग करते और सुनते रहते हैं, पर होता वह सब कुछ खोखला ही है। लोग पूजा- पाठ के कर्मकाण्डों, तीर्थ- पर्यटनों भजन- प्रदर्शन की विडम्बनाओं से मन बहलाते और अपने को धर्मध्वजी मानते देखे गए हैं पर बात वस्तुत: वैसी है नहीं। कर्मकाण्डों का एक मात्र मंतव्य यह है कि चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक शालीनता का समावेश करें। जिन्हें धर्म में वस्तुतः: कुछ रुचि है, उन्हें देवोपम स्तर का जीवनयापन करते देखा जाना चाहिए। उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रामाणिकता एवं प्रखरता से भरे होने चाहिए। अनौचित्य को अपनाकर भी लोग सुविधा- साधनों का संग्रह और चारण- चाटुकारों के माध्यम से मिल सकने वाली प्रशंसा बटोर लेते हैं, पर उनमें न तो यह गहराई होती है न स्थिरता। धुएँ से बने बादल कितने ही घने क्यों न हों, हवा के एक झोंके में जिधर- तिधर बिखर जाते हैं। छलावा पानी के बबूले की तरह कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व गँवा बैठता है।
प्रतिभा के विपुल भंडार मनुष्य की अंत:सत्ता में भरे पड़े हैं, उन्हें उभरने- प्रकट होने का अवसर उन दबावों के कारण आने ही नहीं पाता, जो कषाय- कल्मषों के रूप में आत्मसत्ता के ऊपर स्वेच्छापूर्वक लाद लिए गए हैं। लकड़ी को पानी पर तैरते रहना चाहिए, पर यदि उस पर भारी चट्टानें बाँध दी जाएँ तो अपना स्वाभाविक गुण तैरना दबकर रह जाता है। विभूतिवान् होते हुए भी मनुष्य निकृष्टता की चट्टान सिर पर लाद लेने के उपरांत तैरने और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा पाने की स्थिति में रह ही नहीं जाता।
प्रसुप्त प्रतिभा को जागरण का अवसर मिले, इसके लिए आवश्यक है कि श्रेष्ठ चिंतन से अंतराल को और दुष्ट आचरण से काय कलेवर को बचाए रहने का प्रयत्न किया जाए। यह तभी बन पड़ेगा जब अवांछनीय महत्त्वाकाँक्षाओं की हथकड़ी- बेड़ी से हाथ पैर खुले रहें। लोगों की उत्कंठा धनाढ्य बनने में रहती है, ताकि विलासिता के विपुल साधन जुटाए जा सकें, साथ ही अभावग्रस्तों की बिरादरी में अपने को बढ़ा- चढ़ा सिद्ध करने की मूँछें मरोड़ी जा सकें। इतनी छोटी सीमा में जिनका अंतराल केंद्रीभूत होकर रह गया हैं, वे उन महान् कार्यों के प्रति उन्मुख ही नहीं हो सकते, जो मानवी गरिमा में चार चाँद लगाते हैं। खूँटे से बँधी हुई नाव चप्पू चलाते रहने पर भी आगे कहाँ बढ़ पाती है। संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित व्यक्ति न तो आदर्शवादिता अपना सकता है और न ऐसा कुछ कर सकता है, जिसे उत्कृष्ट कहा जा सके। सज्जा की विडंबना रचकर तो कुरूप वेश्याएँ भी अपने को परी जैसी सुंदर दिखाने का भ्रम रचती रहती हैं।
प्रतिभा कहीं बाहर से बटोरनी नहीं पड़ती, उसे सदा भीतर से ही उभारा जाता है। इसके लिए उन अवरोधों को हटाना अनिवार्य हैं, जो भारी चट्टान की तरह उत्कृष्टता के मार्ग में भयानक अवरोध बनकर अड़े होते हैं। इस संदर्भ में स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अंगीकार किया जाए, अन्यथा तृष्णा और वासना की लिप्सा इतनी सघनता के साथ छाई रहेगी कि अपनी सामर्थ्य की तुलना में अकिंचन जितना परमार्थ भी करते न बन पड़ेगा। यह खाइयाँ इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है कि छोटे- से जीवन का समूचा साधन, श्रम, कौशल खपा देने पर भी उन्हें भरा नहीं जा सकता। फिर वह बन ही कैसे पड़े जो उत्कृष्टता के साथ अति सघनतापूर्वक जुड़े हुए प्रतिभा- परिष्कार का पुण्य- प्रयोजन संतोषजनक मात्रा में उपलब्ध करा सके।
लालसा- जन्य महत्त्वाकाँक्षाओं में कटौती किए बिना किसी के पास भी इतना समय, श्रम, साधन बच नहीं सकता, जिसके सहारे आत्मकल्याण और लोक कल्याण की दिशा में कुछ कहने लायक कदम उठ सकें। साधु और ब्राह्मणों को भूसुर की, पृथ्वी के देवता की उपमा दी जाती रही है। वह इसलिए कि उसने संयम, अपरिग्रह, संतोष की राह अपनाई। अपने निजी बड़प्पन में जिनकी जितनी अभिरुचि होगी, वह उतना ही अपने को व्यस्त और अभावग्रस्त अनुभव करेगा। सदा यही कहता रहेगा कि अपनी समस्याओं से ही घिरा हुआ हूँ, जबकि वस्तुत: वास्तविक समस्याएँ मनुष्यों के सामने होती ही कितनी है? फिर यदि उन्हें व्यावहारिक बुद्धि द्वारा समझदारी के साथ सुलझाया जाए, तो इतनी सरलतापूर्वक सुलझ जाती हैं, मानों वे वस्तुतः: थीं ही नहीं। भ्रांतियों के कारण वे बढ़ी या लाद दी गई हैं।
संयम- नियम के कितने ही अनुबंध हैं, जिनमें आहार- विहार की शुद्धि, सज्जनता, सद्भावना, श्रमशीलता, मितव्ययिता, स्वच्छता, सहकारिता, अनुशासन, प्रियता आदि प्रमुख हैं। इनके विपरीत अनेक दोष हैं- असंयम चटोरपन, आलस्य, प्रमाद, निष्ठुरता, स्वच्छंदता, अपव्यय, व्यसन आदि जो प्रगति में बाधक बनते हैं। यह सब देखने- सुनने में बहुत ही दुष्कर प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः: हैं संकीर्ण स्वार्थपरता और स्वेच्छाचार की पैदा की हुई औलाद ही। इनमें से एक- एक को गिनना और रोकथाम करना मेंढक तोलने के समान है। बिस्तर को धूप में डाल देने के उपरांत खटमल और उनके अंडे- बच्चे सभी मर जाते हैं। इसी प्रकार दृष्टिकोण को उदात्त बना लेने के उपरांत अपना स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य तीनों ही सूझ पड़ते हैं। उस प्रकाश के जलते ही उन भूत- पलीतों से छुटकारा मिल जाता है, जो अँधेरे के कारण सामान्य होते हुए भी, डरावने बनकर भयभीत करते और त्रास देते थे।
दृष्टिकोण में जब विशालता का समावेश होता है तो लगता है कि परमार्थ ही परम स्वार्थ है। इसके बराबर लाभ और किसी व्यवसाय में नहीं। इस तथ्य को इतिहास प्रसिद्ध सभी महामानवों से लेकर सामयिक श्रद्धाभाजन व्यक्तियों के ऊपर बरसती हुई सद्भावना को देखकर सहज समझा जा सकता है, कि व्यक्तिगत लाभ की बात सोचने वाले भी यदि दूरदर्शी हों, तो उन्हें परमार्थ प्रयोजनों में अपनी क्षमता लगाने के उपरांत बदले में कई गुना होकर लौटता है। यही नीति महामानवों की रहती है। वे समाज के खेत में पुण्यपरमार्थ के बीज बिखेर देते हैं और उस फसल को अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी काटते व विश्ववसुधा को लाभान्वित करते हैं। यही प्रतिभा का चिह्न है।
प्रतिभा, तेजस्विता को कहते हैं। यह चेहरे की चमक या चतुरता नहीं, वरन् मनोबल पर आधारित ऊर्जा है। गाँधी जी ९२ पौंड वजन और ५ फुट २ इंच के थे। रंग के काले और कुरूप भी, पर उनका तेजस् ऐसा था कि जनसाधारण से लेकर देश के वरिष्ठ मूर्द्धन्यों तक को उनका आदेश शिरोधार्य करते देखा जा सकता था। यहाँ तक कि विशाल साम्राज्य के अधिपति अंग्रेज भी उनसे प्रभावित होकर बिस्तर गोल करके चले ही गए। यह तेजस् निजी और सामूहिक जीवन के हर पक्ष को जगमगाता है। उसे प्रखरता भरी ऊर्जा से जाज्वल्यमान बना देता है।
तेजस्विता तपश्चर्या की उपलब्धि है, जो निजी जीवन में संयम- साधना और सामाजिक जीवन में परमार्थपरायणता के फलस्वरूप उद्भूत होती हैं। संयम अर्थात अनुशासन का, आत्मनियंत्रण कठोरतापूर्वक परिपालन। इसके लिए मनुष्य को तृष्णा, वासना और अहंता के त्रिविध नागपाशों से छूटता पड़ता है। ‘सादा जीवन उच्च विचार’ का ब्राह्मणोचित औसत नागरिक स्तर का जीवनयापन करना पड़ता है। जो इतना कर सके, उन्हीं से परमार्थ सधता है और योगियों में पाई जाने वाली सिद्धियों, शक्तियों और विभूतियों का अंतराल में उद्भव और अखिल अंतरिक्ष से अभिवर्षण होता है। दैवी अनुग्रह या वरदान भी इसी को कहते हैं।
कर्मकाण्डपरक इसके साधना- विधान अनेक हैं, पर सर्वसुलभ प्रक्रिया यही है कि निजी जीवन इतना हलका- फुलका रखा जाए कि उसका निर्वाह न्यूनतम श्रम और समय में ही संभव होता रहे। इसके उपरांत ही श्रम, समय और साधन इतनी मात्रा में बच पाते हैं कि उनके आधार पर परमार्थ में निरत रहकर परब्रह्म के साथ एकात्म होने का रसास्वादन किया जा सके, देवोपम जीवन जीने का आनंद लाभ उठाया जा सके।
किस प्रयोजन के लिए, किस अवसर पर, किस प्रकार, क्या संयम बरता जाय? यह निर्णय- निर्धारण व्यक्ति विशेष की परिस्थिति और मनःस्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। जिसके जीवन का जो पक्ष उद्धत हो चला हो, उसे सरकस के जानवरों की तरह बलचातुर्य प्रयोग करते हुए कलाकौशल दिखा सकने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। शरीर और मन दोनों को ही शालीनता अपनाए रहने के अभ्यस्त करना पड़ता है। संयम योग यही है। जो इतना कर सका, वही पुण्य- परमार्थ अर्जित करने का भी अधिकारी है। उद्धत आचरण वाला व्यक्ति कीचड़- से धोने के प्रयत्न में क्या कुछ सफलता प्राप्त कर सकेगा? शालीनता और परमार्थपरायणता मिलकर ही तपश्चर्या बनती हैं और उन्हीं के आधार पर प्रतिभा की ऊर्जा अपनी प्रचंडता का परिचय देती है।
Versions
-
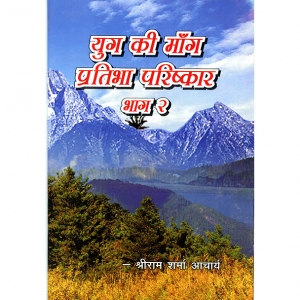
HINDIयुग कि मांग प्रतिभा परिष्कार भाग-२Scan Book Version
-
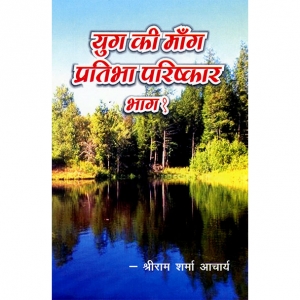
HINDIयुग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग-१Scan Book Version
-

ENGLISHRefinement of Talents: Need of the present EraScan Book Version
-
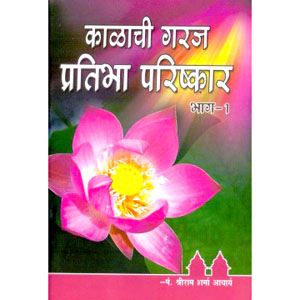
MARATHIकालाची गरज प्रतिभा परिष्कार भाग 1Scan Book Version
-

MARATHIकालाची गरज प्रतिभा परिष्कार भाग 2Scan Book Version
-
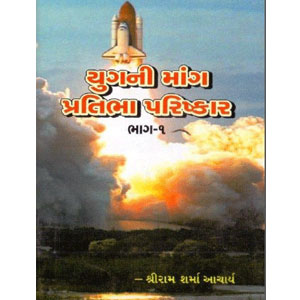
GUJRATIયુગની માંગ પ્રતિભા પરિષ્કાર ભાગ - ૧Scan Book Version
-
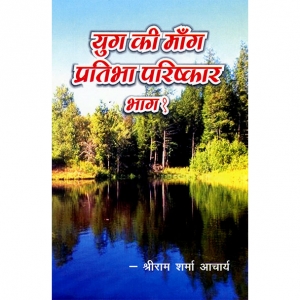
HINDIयुग की माँग प्रतिभा परिष्कार-भाग १Text Book Version
-
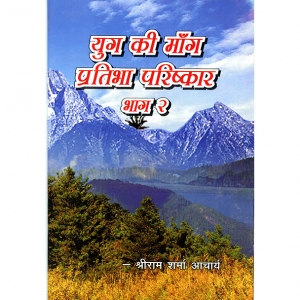
HINDIयुग की माँग प्रतिभा परिष्कार-भाग २Text Book Version
-
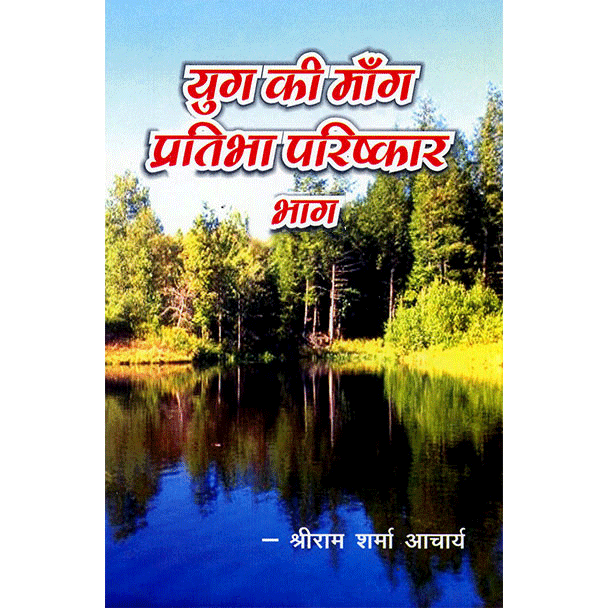
HINDIयुग की माँग प्रतिभा परिष्कारText Book Version

