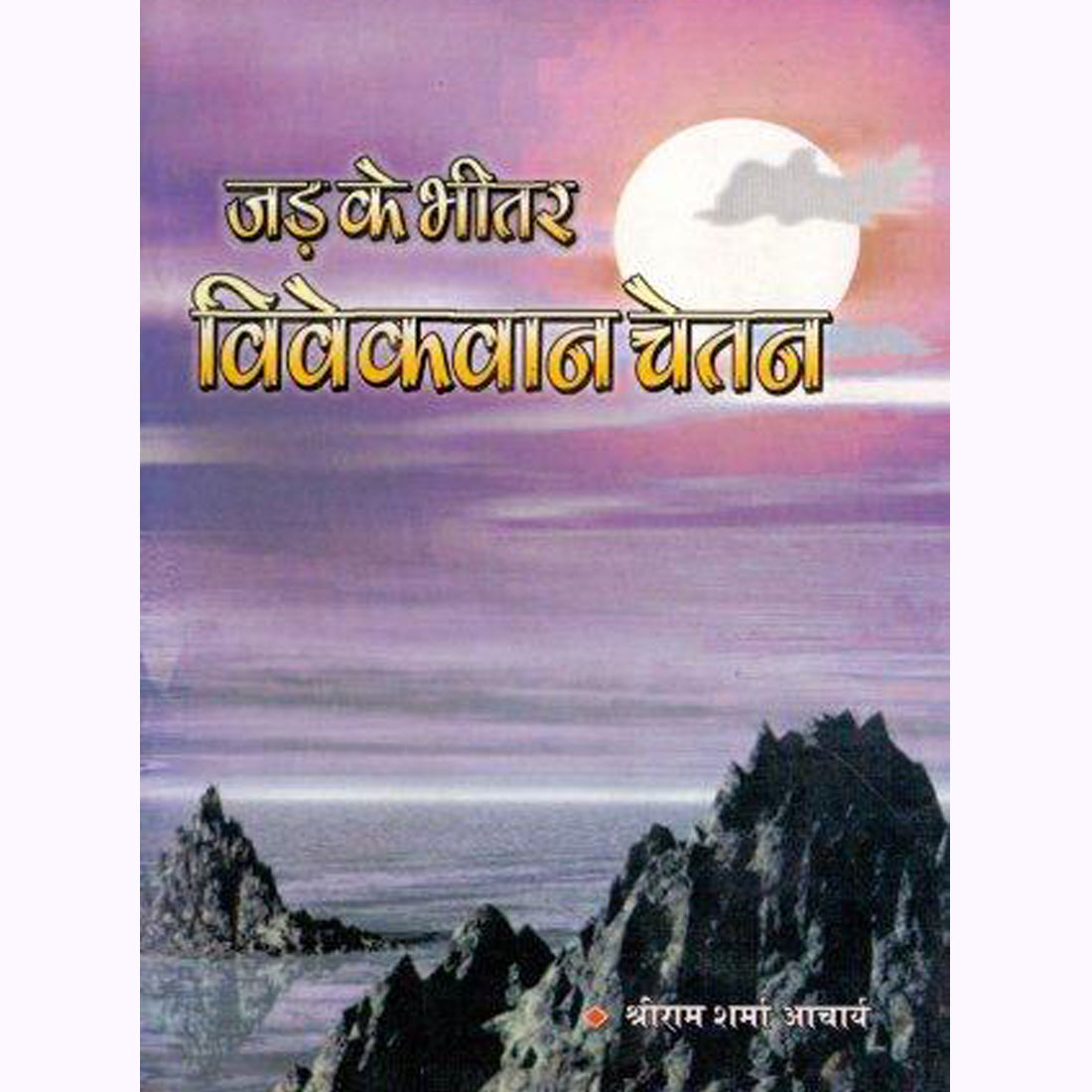जड़ के भीतर विवेकवान चेतन 
प्रकृति की जीवन व्यवस्था
Read Scan Version
दृश्य प्रकृति में जो कुछ भी है अच्छी और बुरी दो प्रवृत्तियों में बंटा हुआ है। जीवन की सूक्ष्मतम अवस्था जीवाणु का अध्ययन करें तो एक दूसरा तथ्य भी उपस्थित होता है वह यह कि अच्छाइयां और बुराइयां किसी और की देन नहीं यह भी स्वयम्भू हैं। मनुष्य का अपना देवत्व ही अच्छी प्रवृत्तियां विकसित कर लेता और उनके सत्परिणामों से लाभान्वित होता है जब कि उसका अन्तः पिशाच ही दुष्प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट हो उठता और न केवल उसे अपितु दूसरों का भी सर्वनाश करके छोड़ता है। जीवाणु अर्थात् देवत्व की शक्ति, प्रति जीवाणु या विषाणु असुरता का प्रतीक है।
सल्यूलोग आवरण से आच्छादित तरल प्रोटोप्लाज्मा से बने जीवाणु किसी भी स्थान पर नमी, आदि पाकर स्वयं ही जन्म ले लेते हैं यह इतनी सूक्ष्म सत्ता है कि एक इंच की लम्बी लकीर में इन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाये तो 25000 जीवाणु बड़े मजे में खड़े हो जायेंगे। इतनी आदमी एक पंक्ति में खड़े किये जायें और यह माना जाये कि एक व्यक्ति औसतन 1 फुट जगह लेगा तो कुल आदमियों के लिए 5 मील लम्बी सड़क आवश्यक होगी। देवत्व सूक्ष्म तत्व है अनुभूति के लिए वैसी ही सूक्ष्म बुद्धि दूरदर्शी समीक्षा चाहता है यह न हो तो मनुष्य सामान्य स्वार्थ को ही उस श्रेणी में मानकर उसके लाभों से वंचित हो सकता है।
विषाणु तो उससे भी सूक्ष्म और प्रभावी सत्ता है एक इंच में यह 141000 आसानी से बैठ सकते हैं—अर्थात् यदि वह आदमी बराबर हों और यह माना जाये कि उनमें से प्रत्येक को 1 फुट ही जगह चाहिए तो 26 मील सड़क की आवश्यकता होगी। तात्पर्य यह हुआ कि बुराई की शक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है। वह अब आ धमके यह पता लगाना भी कठिन है जब तक कि उतनी ही पैनी और सूक्ष्म निरीक्षण बुद्धि न रखें।
जीवाणु जल में भी होते हैं और इस रूप में वे लोकसेवी हमारे जीवन के पोषक के रूप में काम करते हैं। मिट्टी में पड़े मल और सड़न को बैक्टीरिया ही खाकर उसे अच्छी मिट्टी में बदलते रहते हैं। देव-प्रवृत्तियां भी इसी तरह अपने को बढ़ाने में सहायक होती हैं। साथ ही वह सृष्टि के उच्छिष्ट तत्व सड़ाकर सब को नष्टकर स्वच्छ, पवित्र वातावरण बनाती है। जिससे सर्वत्र सुख-शान्ति और प्रसन्नता बढ़ती है। जीवाणु 10 या 20 मिनट में ही अन्य जीवाणुओं को जन्म देने लगते हैं और 24 घण्टे में 17000000 जीवाणुओं में परिणत हो जाते हैं। देवत्व एक क्षण के लिए भी उदित हो तो दूरगामी शान्ति और व्यवस्था की नींव गहरी जमा जाता है।
दूसरी ओर विषाणु है जो जीवाणु के ही पैरों में लगा चला आता है। बुराइयां सदैव छद्म वेष में देवत्व के बाने में आती हैं अन्यथा उन्हें स्थान ही न मिले इसलिए अच्छाइयां जहां हमारे जीवन को अभीष्ट हैं। वहीं सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अतिथि और मित्र बनकर आये परिजनों में ही कहीं कोई अपनी द्विविधा और भ्रम का लाभ उठाकर कोई चोर उचक्का तो नहीं आ धमकता।
दूध में पड़ा बैक्टीरिया उसे दही बना देता है देवत्व और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति समाज को भी उसी तरह सुन्दर बना देती है, जैसे दूध की अपेक्षा दही अधिक सुपाच्य हो जाता है। अपने जीवन में छोटी से छोटी वस्तु का उपयोग है। यदि हम भलाई के हर कण को अपनाने की कला सीख जायें तो हर किसी के आदर और विश्वास के पात्र बन सकते हैं, पर विषाणु जहां भी पहुंच जायें वहीं बीमारी पैदा कर दें अर्थात् बुराई के कर्म ही नहीं विचार भी हमारे पतन का आधार बन जाते हैं।
जीवाणु तथा विषाणु दोनों की ही संचार और विस्तार व्यवस्था बड़ी व्यापक है, पक्षियों के परों में लिपटे जहाजों में चढ़ कर यात्रियों के माध्यम से भी ये एक स्थान-से एक देश से, दूसरे स्थान-दूसरे देश पहुंच जाते हैं। और सर्वत्र महामारी की स्थिति पैदा कर देते हैं कुछ न मिले तो हवा ही उनके लिए उपयुक्त वाहन है। इसी से यह कहीं भी जा पहुंचते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों का क्षेत्र भी उसी तरह सर्वत्र खुला पड़ा है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अर्वाचीन युग के देवत्व की भी अपने वर्तमान जीवन में बुला सकते हैं और नाटकों, फिल्मों से भी अच्छे बनने की प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरों के अच्छे आचरण हमारे जीवन दीप बन सकते हैं। और उनकी शिक्षायें भी वही प्रेरणा दें सकती हैं। बुराइयों के लिए भी ठीक यही स्थिति है बुलायें तो मन ही मन से करोड़ों मनोविकार आमन्त्रित करलें दृढ़ता हो तो दृष्टि में पड़ने वाली कुत्सा भी अन्दर झांकने न पाये।
हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्तियां जड़ न जमा पायें उसके लिए उन्हें मारने की मुहीम जाग्रत रखनी चाहिए। एण्टी बायटिक औषधियां जिस तरह शरीर में पहुंच कर वहां के विषाणुओं को चारों ओर से घेर कर रसद मार्ग काट कर उन्हें आत्मघात को विवश करती हैं, उसी तरह आत्म सुधार के लिए हमें प्रलोभनों को मार भागने का—बुराइयों से लड़ने का माद्दा अपने अन्दर से ही पैदा करना चाहिए। यदि ऐसा करलें तो वह हमारी उसी तरह हानि नहीं कर सकतीं जिस तरह हास्पिटलों में टी.बी., कैन्सर आदि के मरीज भरे पड़े रहते हैं। स्वाभाविक है कि वहां विषाणुओं का सरोवर लहरा रहा हो किन्तु उसी वातावरण में डॉक्टर लोग दिन-दिन भर काम करते रहते हैं। फिर भी उनका रत्ती भर भी अहित नहीं हो पाता।
दैवी अंश प्रबल हों तो वह सशक्त जीवाणुओं की तरह शरीर की ढाल का कार्य करते हैं। उससे असुरता हावी नहीं होने पाती, आत्म सुधार की सबसे अच्छी प्रक्रिया यह है कि हम निरन्तर रचनात्मक विचारों को मस्तिष्क में विकसायें, रचनात्मक कार्य करते रहें उससे बुराइयां अपने आप ही झांक कर लौट जाती हैं। जिस घर में पहले ही समर्थ लोग रहते हों वहां चोर उचक्के झांक कर ही लौट जाते हैं।
लेकिन यदि सीलन, सड़न, गलन अपने भीतर ही हो तो कमजोर भले मानस को भी सशक्त बदमाशों द्वारा सताये जाने की तरह बुराइयों को पनपने का भीतर ही आधार मिल जायेगा। बाहर के विषाणु शरीर में आयें पर शरीर सशक्त हो, पाचन यन्त्र ठीक काम करते हों, रुधिर में श्वेताणुओं की कमी न हो तो विषाणु रत्ती भर असर नहीं डाल पायेंगे उल्टे नष्ट हो जायेंगे पर भीतर विजातीय द्रव्य भरा हो, आदमी में आकर्षणों की सड़न भीतर-भीतर बुश रही हो तब तो वे अपनी शक्ति भीतर ही बढ़ा कर हमारे विनाश का कारण बन जायेंगे यहीं नहीं विजातीय द्रव्य के बाद वे शरीर की कोशाओं को भी खाने लगेंगे तब फिर जीवन का अन्त होगा ही।
प्रकाश में विषाणुओं को मार देने की शक्ति है। हमारे जीवन में प्रकाश तत्व बना रहे—विवेक बना रहे तो न केवल भलाई की शक्ति—देवत्व का विकास और उसके फलितार्थों से लाभान्वित होते रह सकते हैं। आसुरी तत्व वे चाहे कितने ही अदृश्य और शक्ति शाली क्यों न हों जानकारी में आते रहें और उन्हें नष्ट करने मार कर भगा देने का साहस हमारे जीवन में बना रहना चाहिए।
प्राणी यों प्रकृति की विपरीत चपेट में आकर अक्सर अस्तित्व गंवा बैठता है। नियति के उग्र परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाता और विपरीत परिस्थिति के सामने अपने को निरीह असमर्थ अनुभव करता है, पर ऐसा तभी होता है जब वह उस आपत्ति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार न हो। यदि प्राणी को विपरीत अनभ्यस्त परिस्थिति में रहने को विवश होना पड़े तो वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए क्रमशः ऐसे परिवर्तन उत्पन्न कर लेता है—ऐसी विशेषता का उत्पादन कर लेता है जिसके आधार पर वह प्राणघातक समझी जाने वाली परिस्थितियों से भी तालमेल बिठा ले और अपना अस्तित्व कायम रख सके, सुविधा पूर्वक निर्वाह कर सके।
जीवाणुओं की असह्य तापमान पर मृत्यु हो जाती है। वे अधिक उष्णता एवं शीतलता सहन नहीं कर सकते, यह मान्यता अब पुरानी पड़ चली है। पानी खौलने से अधिक गर्मी और 270 आ. से. नीचे शीत पर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाने की बात ही अब तक समझी जाती रही है। इसका कारण यह था कि शरीर में पाया जाने वाला ग्लिसरोद रसायन असह्य तापमान पर नष्ट हो जाता है और जीवाणु दम तोड़ देते हैं अब वे उपाय ढूंढ़ निकाले गये हैं कि इस रसायन को ताप की न्यूनाधिकता होने पर भी बचाया जा सके और जीवन को अक्षुण्ण रखा जा सके।
अत्यधिक और असह्य शीतल जल में भी कई प्रकार के जीवित प्राणी निर्वाह करते पाये गये हैं इनमें से प्रोटो—जुआ, निमैटौड, क्रस्टेशिया, मोलस्का आदि प्रमुख हैं। येलोस्टोन की प्रयोगशाला में लुइब्राक और टामस नामक दो सूक्ष्म जीव-विज्ञानी—माइक्रो वायोलाजिस्ट यह पता लगाने में निरत हैं कि जीव सत्ता के कितने न्यून और कितने अधिक तापमान पर सुरक्षित रह सकने की सम्भावना है। वे यह सोचते हैं कि जब पृथ्वी अत्यधिक उष्ण थी तब भी उस पर जीवन सत्ता मौजूद थी। क्रमश ठण्डक बढ़ते जाने से उस सत्ता ने क्रमिक विकास विस्तार किया है, पर इससे क्या—अति प्राचीन काल में जब जीवन सत्ता थी ही तो वह विकसित अथवा अविकसित स्थिति में अपनी हलचलें चला ही रही होगी भले ही वह अब की स्थिति की तुलना में भिन्न प्रकार की अथवा पिछड़े स्तर की ही क्यों न रही हो। विकसित प्राणी के लिए जो तापमान असह्य है वह अविकसित समझी जाने वाली स्थिति में काम चलाऊ भी हो सकता है।
यदि यही तथ्य हो तो फिर जीवन की मूल मात्रा को शीत, ताप के बन्धनों से युक्त माना जा सकता है और गीताकार के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मा को न आग जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न जल डुबा सकता है। पंचभूतों की प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए वह अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकने में पूर्णतया समर्थ है।
समुद्र तट के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली धूसर रंग की मक्खी ‘एफिड्रिल को 45 डिग्री से 51 डिग्री से. के बीच तापमान वाले गर्म जल में प्रवेश करते देखा गया है। यह प्राणियों के जीवित रहने को असम्भव बनाने वाले गर्मी है। सामान्यतया धरती की सतह पर 21. से. तापमान रहता है। प्राणियों को उतना ही सहन करने का अभ्यास होता है। अधिक उष्ण या अधिक ताप के वातावरण में रहने वाले जन्तुओं को विशिष्ठ स्थिति के अभ्यस्त ही कह सकते हैं।
एफिड्रिड मक्खी के अतिरिक्त कुछ जाति के बैक्टीरिया भी ऐसे पाये गये हैं जो खौलते पानी के 92 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान में भी मजे से जीवित रहते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित गर्म जल के झरने प्रायः इसी तापमान के हैं और उनमें जीवित बैक्टीरिया पाये गये हैं। इन गर्म झरनों अथवा कुण्डों में एक प्रकार की काई सी मोटी परत जमी रहती है जिसे हिन्दी में शैवाल कहा जाता है अंग्रेजी में उसका नाम एल्गी है। इसमें जीवन रहता है। आमतौर से वह 75 डिग्री से. तक गर्म जल में मजे का निर्वाह करती है बैक्टीरिया उसी के सहारे पलते हैं। एफिडिड मक्खी के, प्रमुख भोजन यह एल्गी ही है उस प्राप्त करने के लिए वह उस असह्य तापमान के जल में डुबकी लगाती है और बिना जले, झुलसे अपना आहार उपलब्ध करती है।
यह तो हुई छोटे जीवों की बात, अब अधिक कोमल समझे जाने वाले मनुष्यों की बात आती है वह भी प्रकृति की असह्य कही जाने वाली स्थिति में निर्वाह करने के लिए अपने को ढाल सकता है। उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहने वाले एक्सिमो लोग अत्यधिक शीत भरे तापमान में रहते हैं। भालू, हिरन और कुत्ते भी उस क्षेत्र में निवास करते हैं। वनस्पतियां और वृक्ष न होने पर पेट भरने के लिए मांस प्राप्त कर लेते हैं इसके लिए उसने बर्फ की मोटी परतें तोड़ कर नीचे बहने वाले समुद्र में से मछली पकड़ने की अद्भुत कला सीखली है आयुध साधन रहित होते हुए भी हिरन, भालू और कुत्तों का भी वे शिकार करना सीख गये हैं और लाखों वर्ष से उस क्षेत्र में निर्वाह कर रहे हैं।
प्रकृति के अनोखे वरदान
पैस्फिक सागर में गोता लगाकर मोती ढूंढ़ने वालों को पता चला कि ‘‘स्टार फिश’’ (यह तारे की तरह चमकने वाली छोटी सी मछली होती है) ही अधिकांश सीपियों को नष्ट कर डालती है अतएव वे मोती ढूंढ़ने से पहले इन स्टारफिशों को ही समूल नष्ट कर डालने के लिये जुट पड़े। उन्होंने इन्हें पकड़ पकड़ कर काटना शुरू कर दिया। एक, दो, दस, पचास, सैकड़ा हजार—कितनी ही स्टारफिशें काट डाली गईं पर रावण के मायावी सिरों की भांति वे कम न हुईं उलटे उनकी संख्या बढ़ती ही गई। अभी तक तो उनकी उपस्थिति ही चिन्ताजनक थी अब तो उनकी आश्चर्यजनक वृद्धि और भी कष्टदायक हो गई अन्त में यह जानने का फैसला किया गया कि आखिर यह स्टारफिशों की वृद्धि का रहस्य क्या है?
सावधानी से देखने पर पता चला कि जो स्टारफिश काट डाले गये थे उनका प्रत्येक टुकड़ा स्टारफिश बन चुका था अभी तक अमीबा, हाइड्रा जैसे एक कोशीय जीवों के बारे में ही यह था कि ये अपना ‘‘प्रोटोप्लाज्म’’ दो हिस्सों, दो से चार चार से आठ हिस्सों में बांटकर वंश वृद्धि करते जाते हैं पर अब इस बहुकोशीय जीव को काट देने पर भी जब एक स्वतंत्र अस्तित्व पकड़ते देखा गया तो जीव शास्त्रियों का प्रकृति के इस विलक्षण रहस्य की ओर ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। तब से निरन्तर शोध-कार्य चलता रहा। और देखा गया कि नेस सलामैसीना, आइस्टर, स्नेल (घोंघा फ्रेश वाटर मसल (शम्बूक) साइलिस, चैटोगैस्टर स्लग मन्थर) पाइनोगोनाइड (समुद्री मकड़ी) आदि कृमियों में भी यह गुण होता है कि उनके शरीर का कोई अंग टूट जाने पर हो नहीं वरन् मार दिये जाने पर भी वह अंग या पूरा शरीर उसी प्रोटोप्लाज्म से फिर नया तैयार कर लेते हैं। केकड़ा तो इन सबमें विचित्र है। टैंक की सी आकृति वाले इस जीव की विशेष यह है कि अपने किसी भी टूटे हुए अंग को तुरन्त तैयार कर लेने की प्रकृति दत्त सामर्थ्य रखता है।
यह तथ्य जहां इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इच्छा शक्ति पदार्थ का बन्धन रहित उपयोग कर सकने में समर्थ है वहां इस बात को भी प्रमाणित कर रहे हैं कि आत्म चेतना एक शक्ति है और वह भौतिक शक्तियों से बिलकुल भिन्न मरण-धर्म से विपरीत है। उस पर जरा, मृत्यु आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्म तत्व भले ही वह किसी भी घृणित और तुच्छ से तुच्छ वासना एवं इच्छा शक्ति के रूप में क्यों न हो, इतना सशक्त है कि स्वेच्छा से न केवल अपने भीतर से उत्पादन की क्रिया आप ही करता रहता है वरन् अपने पूर्णतया मुर्दा शरीर को भी बार-बार जीवित और नया कर सकता है। इन महान आश्चर्यों को देखकर ही लगता है भारतीय तत्व:दर्शियों ने सृष्टि विकास क्रम को ईश्वर इच्छा शक्ति पर आधारित माना। इसी आधार पर विकासवाद जैसा सिद्धान्त विखण्डित हो जाता है। जब प्रकृति के नन्हे-नन्हे जीवन, उत्पादन, उत्पत्ति और विकास की क्रिया में समर्थ होते हैं तो कोई एक ऐसा विज्ञान भी हो सकता है जब कोई एक स्वतन्त्र इच्छा शक्ति अपने आप पंच महाभूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश) के संयोग से अपने आपको प्रकट कर दें यों देखने में यह क्रिया बीज और वंशानुगत होती प्रतीत होती है।
हाइड्रा देखने में ऐसा लगता है जैसे एक स्थान पर फूल-पत्ते इकट्ठा हों। उसके अंग की कोई एक पंखुड़ी एक ओर बढ़ना प्रारम्भ होती है और स्वाभाविक वृद्धि से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह अधिक बढ़ा अंग अपने आपको मूल भाग से अलग कर लेता है और वह एक स्वतन्त्र अस्तित्व बन जाता है। पैरामीशियम, यूग्लीना आदि एक कोशीय जीवों में प्रजनन का यही नियम है जो यह बताता है कि आत्म-सत्ता को एक सर्वांगपूर्ण शरीर यन्त्र के निर्माण के लिये करोड़ों वर्षों के विकासक्रम की आवश्यकता या प्रतिबन्ध नहीं हैं यदि उसे अपने लघुत्तम या परमाणिविक स्वरूप का पूर्ण अन्तःज्ञान हो जाय तो वह कहीं भी कैसा भी रूप धारण करने में समर्थ हो सकता है। सम्भवतः अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा यह सिद्धियां इसी तथ्य पर आधारित हैं। एक दिन विज्ञान भी इस दिशा में सफल हो सकता है, वह स्थिति आ सकती है, जब सम्मोहन शक्ति के द्वारा रासायनिक ढंग से उत्पादित प्रोटोप्लाज्मा में जीवन उत्पन्न किया जा सके। कैसा भी हो इस महान् उपलब्धि के लिये विज्ञान को पदार्थ तक ही सीमित न रहकर ‘‘भाव’’ को भी संयुक्त करना ही पड़ेगा जैसा कि भारतीय तत्व वेत्ताओं ने अब से हजारों वर्ष पूर्व कर लिया था।
स्टेन्टर अपने प्रोटोप्लाज्मा का 1/60 अंश बाहर का देता है और उसी से एक नया स्टेन्टर तैयार कर देता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा को नयी सन्तान पैदा करने के लिये अपने शरीर का कुल 1/300 वां हिस्सा पर्याप्त है।
प्राणों को जिस प्रतिभा का लाभ मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के रूप में मिला, सृष्टि के अन्य प्राणी भी उस प्राण की महत्ता से सृष्टि के नन्हें-नन्हें जीव भी अनभिज्ञ नहीं। बेशक वह प्राणों के स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकते, प्राणों का असीमित विकास और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली तेजस्विता, दीर्घजीवन प्रज्ञा बुद्धि का लाभ नहीं ले सकते पर उनमें भी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि वे अपने मृत शरीर का बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। परकाया प्रवेश की क्षमता भारतीय योगी ही अर्जित कर सके हैं पर प्रकृति में ऐसे अनेकों योनी हैं जो अपने ही मरे, कुचले टूटे फूटे शरीर का अपने प्राणों के बल पर पुनः उपयोग कर लेते हैं।
जीवित स्पंज को लेकर टुकड़े-टुकड़े कर डालिये, उससे भी मन न भरे तो उन्हें पीसकर पीसकर कपड़े से छान लीजिये। पिसे और कूट कपड़छन किये शारीरिक द्रव्य को पानी में डाल दीजिये। शरीर के सभी कोश धीरे-धीरे फिर एक स्थान पर मिल जायेंगे और कुछ दिन बाद पूरा नया स्पंज फिर से अपनी जीवन यात्रा प्रारम्भ कर देगा। चुनौती है स्पंज की कि जब तक प्राण हैं तब तक मुझे शरीर के अवसान की कोई चिन्ता नहीं। मरना जीना तो मात्र प्राणों का ही खेल है।
हाइड़ा, स्टेन्टर तथा प्लेनेरिया आदि जीवों में यह गुण होता है कि वे अपने शरीर के एक छोटे से अंश को (300 वें भाग तक छोटे टुकड़े को) ही तोड़कर नया शरीर बना देते हैं उन्हें गर्भ धारण भ्रूण-विकास और प्रजनन जैसी परेशानियां उठानी नहीं पड़तीं। लगता है प्राण-तत्व की जानकारी होने के कारण ही प्राचीन भारत के तत्वदर्शी एक भ्रूण से 100 कौरव, घड़े से कुंभज और जघा से सरस्वती पैदा कर दिया करते थे। अन्य एक कोशीय जीवों में पैरामीशियम तथा यूग्लीना में भी एक कोश से विभक्त होकर दूसरा स्वस्थ कोश अर्थात् नया जीव पैदा कर देने की क्षमता होती है। यह घटनायें इस बात की साक्षी भी हैं कि ऐसी क्षमतायें अणु जैसी सूक्ष्म मनःस्थिति तक पहुंचने वाली क्षमता से ही प्रादुर्भूत हो सकती है।
टूटे हुए शारीरिक अंगों के स्थान पर नये अंग पैदा कर लेने की क्षमता ही कुछ कम विलक्षण नहीं ट्राइटन सलामाण्डर, गोह अपने कटे हुए शरीर को क्षति पूर्ति तुरन्त नये अंग के विकास रूप में कर लेते हैं। अमेरिका, अफ्रीका में पाये जाने वाला शीशे का सांप जरा-सा छूने से टूट जाता है पर उसमें यह भी विशेषता होती है कि अपने टूटे हुये अंग को पुनः जोड़ लेता है। आइस्टर, शम्बूक घोंघा, समुद्री मकड़ी, मन्थर आदि जीवों में भी यह गुण होते हैं। स्टारफिश के पेट में कोई जहरीला कीड़ा चला जाये तो वह अपना पूरा पेट ही बाहर निकाल कर फेंक देती है और नया पाचन संस्थान तैयार कर लेती है सलामेसिनानेस, साहलिस तथा काटो मास्टर जीव तो स्पंज की तरह होते हैं उन्हें कितना ही मार डालिये, मरना उनके लिये जबर्दस्ती प्राण निकाल देने के समान होता है जहां दबाव समाप्त हुआ यह अपने प्राणों को फिर मरे मराये शरीर में प्रवेश करके जीवन यात्रा प्रारम्भ कर देते हैं।
जीवन यात्रा में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के लिए भी प्रकृति ने मनुष्य देह में समुचित प्रबन्ध कर रखा है। मनुष्य जो कुछ खाता-पीता है उससे जीवनी शक्ति को उसकी सहायता के लिये कार्बोहाइड्रेट, (कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन) चर्बी, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज द्रव्य मिलते हैं। भोजन में से यह आवश्यक तत्व ग्रहण करने के लिये गले की नली से लेकर आमाशय की छोटी आंतों तक ही पूरी मशीन दिन-रात काम करती रहती है। उससे भी अधिक ध्यान और मशीनरी का निर्माण शरीर में इसके लिये किया गया है कि शरीर द्वारा उत्पन्न होने वाली गन्दगी शरीर से अलग होती रहे। भोजन और शक्ति के अभाव में मनुष्य कुछ दिन जी भी सकता है पर स्वच्छता और सफाई के अभाव में मनुष्य शरीर अधिक दिन तक टिक नहीं सकता।
शरीर के वृक्क प्रतिदिन डेढ़ सेर मूत्र निकालते हैं। इसके द्वारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रीटीनाइन, एमोनिया, सोडियमक्लोराइड, फास्फोरिक अम्ल, मैगनीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की बहुत सी गन्दगी शरीर से बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत प्रतिदिन ढेरों मल निकालती रहती है। शरीर की त्वचा में लाखों की संख्या में ग्रन्थियां होती हैं जो रक्त से पसीने को छान कर बाहर निकालती रहती हैं। हथेली के एक वर्ग इन्च में ही ऐसी कम से कम 3600 ग्रन्थियां होती हैं इससे पता चलता है कि प्रकृति ने शरीर में सफाई की व्यवस्था को सबसे अधिक ध्यान देकर सावधानी से जमाया है यदि शुद्धीकरण की यह क्रिया एक दिन को भी बन्द हो जाये तो शरीर सड़ने लगे और मस्तिष्क पागल हो जाये।
शरीर ही नहीं प्रकृति का हर कण और प्रत्येक क्षण दोष दूषणों के प्रति सजग और सावधान रहता है जहां भी कहीं गन्दगी दिखाई दी प्रकृति उस पर टूट पड़ती है और देखते-देखते गन्दगी को साफ करके उस स्थान को शुद्ध और उपयोगी बना देती है।
जिसे हम नगण्य समझते हैं—उस मिट्टी में भी फफूंद (फगाई) एक्टीनो माइसिटीज तथा दूसरे कई महत्वपूर्ण जीवाणु (बैक्टीरिया) पाये जाते हैं। यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें शक्तिशाली खुर्दबीनों माइस्कोप से ही देखा जा सकता है। पर उनकी इस लघुता में वह महानता छिपी है जो सारे मनुष्य समाज के हितों की रक्षा करती है यदि यह जीवाणु न होते यह सारी पृथ्वी 7 दिन के अन्दर पूरी तरह से मल से आच्छादित हो जाती और तब मनुष्य का जीवित रहना भी असम्भव हो जाता।
जैसे ही कोई सड़ी-गली वस्तु, मल या कोई गन्दगी जमीन में गिरी यह जीवाणु दौड़ पड़ते हैं और इन गन्दगी के अणुओं की तोड़-फोड़ प्रारम्भ कर देते हैं। दूसरे दिन हम उधर जाते हैं तो मल के ढेर के स्थान पर मिट्टी का-सा ढेर दिखाई देता है। लोग उपेक्षा से देखकर निकल जाते हैं पर वहां प्रकृति का एक बड़ा उपयोगी सिद्धान्त काम करता रहता है। यह जीवाणु इस गन्दगी के एक-एक अणु को तब तक तोड़ते फोड़ते रहते हैं जब तक वह सारी की सारी मिट्टी में बदल नहीं जाती।
प्रतिरोध की स्वयं समर्थ शक्ति
सरल और सहज जीने की चाह तो हर किसी को रहती है पर उसकी पूर्ति होना शक्य नहीं। प्रकृति चाहती है कि हर प्राणी को—संघर्ष की पाठशाला में पढ़कर शौर्य साहस की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। सरल जीवन में सुविधा तो है, पर हानि यह है कि प्राणी की प्रखरता नष्ट हो जाती है उसकी प्रतिभा अविकसित रह जाती है। प्रतिकूलता से जूझे बिना जीवन के शस्त्र पर धार नहीं धरी जा सकती, चमक और पैनापन लाने के लिए उसे पत्थर पर घिसा ही जाता है। मनुष्य समर्थ, सबल और प्रखर बना रहे इसके लिए संघर्ष रत रखने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। इसी व्यवस्था क्रम में एक भयंकर लगने वाली रोग कीटाणु संरचना भी है जो जीवन को मृत्यु में बदलने के लिए निरन्तर चुनौती देती रहती है।
आंखों से न दीख पड़ने वाले अत्यन्त सूक्ष्म रोग कीटाणु हवा में घूमते रहते हैं—प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के सहारे रेंगते रहते हैं और अवसर पाते ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी वंश वृद्धि आश्चर्यजनक गति से होती है। उनकी विषाक्तता एवं मारक शक्ति भी अद्भुत होती है। शरीर में सांस, जल या दूसरे किन्हीं आधारों पर वे प्रवेश कर जाते हैं और वहां पहुंच कर अपनी गति-विधियों से भयानक रोगों का सृजन करते हैं। उनके प्रतिरोध को प्रकृति ने व्यवस्था की है। रक्त में पाये जाने वाले श्वेत कीटाणु इन शत्रुओं से जूझते हैं। शरीर की गर्मी तथा विभिन्न स्थानों से निकलने वाले स्राव उन्हें मारते हैं। इस युद्ध में बहुधा मनुष्य की जीवनी शक्ति ही विजयी होती है तभी तो स्वास्थ्य रक्षा सम्भव होती है अन्यथा इन विषाणुओं के द्वारा होते रहने वाले अनवरत आक्रमण से शरीर का एक दिन भी जीवित रह सकना सम्भव न हो सके।
इन रोग कीटाणुओं की असंख्य जातियां हैं और उनके क्रिया-कलाप भी अद्भुत हैं। वर्तमान रोग परीक्षापद्धति में यह पता लगाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है कि रोगी के शरीर में किन रोग कीटाणुओं का आधिपत्य है। मल-मूत्र, कफ, रक्त आदि की परख करके इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और तद्नुरूप उन्हें मारने की विशेषताओं वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। विषाणुओं की अनेक जातीय के अनुरूप ही उनकी मारक औषधियां ढूंढ़ी गई हैं। इन्हें एंटी बाइटिक्स कहते हैं। इन दिनों इन औषधियों का निर्माण और उपयोग खूब हो रहा है। रोग निवारण का इन दिनों यह प्रमुख आधार है।
पैनसिलीन स्ट्रेप्टोमायसिन वर्ग की रोग कीटनाशक एन्टी बायोटिक्स औषधियों में अब एक और चमत्कारी चरण जुड़ गया है वह है लैडरली लैवोरेटरी द्वारा प्रस्तुत किया गया रसायन डी. एम-सी. टी.। इसका पूरा नाम है—डिमिथाइल क्लोर टैटरासाइक्लिन, इन दवाओं की चमत्कारी औषधियों को ‘‘वन्डर ड्रग्स’’ कहा जाता है। इनका मूल उद्देश्य है शरीर में उत्पन्न हुए या प्रवृष्ट हुए रोग कीटाणुओं को निरस्त करना। विकृत वैक्टीरियाओं—वायरसों के उपद्रव ही विभिन्न रोगों के प्रधान कारण माने जाते हैं। यह, मारक औषधियां इन कीटकों पर आक्रमण करती हैं—इन्हें मूर्छित करतीं और मारती हैं फलतः रोगों के जो कष्टकारक उपद्रव लक्षण थे वे शमन होते दिखाई देते हैं। इन मारक रसायनों के प्रयोग का उत्साह इसलिए ठंडा हो जाता है कि वे विषाणुओं के मारने के साथ रक्षाणुओं को भी नहीं बख्शती। उनकी दुधारी तलवार बिना अपने पराये का, मित्र-शत्रु का भेद-भाव किये जो भी उनकी पकड़ परिधि में आता है उन सभी का संहार करती है। पैनिसिलीन के चमत्कारी लाभों की आरम्भ में बहुत चर्चा थी, पर जब देखा गया कि उसके प्रयोग से दानेदार खुजली जैसे कितने ही नये रोग उत्पन्न होते हैं और किसी-किसी को तो उसकी प्रतिक्रिया प्राणघातक संकट ही उत्पन्न कर देती है। तब वह उत्साह ठंडा पड़ा। अब कुशल डॉक्टर पेनिसिलीन का प्रयोग आंखें मूंदकर नहीं करते। उसके लिए उन्हें फूंक फूंककर कदम धरना होता है। कुनैन से मलेरिया के जीवाणु तो मरते थे, पर कानों का बहरापन—नकसीर फूटना जैसे नये रोग गले बंध जाते हैं। इस असमंजस ने उसके प्रयोग का आरम्भिक उत्साह अब शिथिल कर दिया है। कुनैन का अन्धाधुन्ध प्रयोग अब नहीं किया जाता।
लन्दन के बारथोलोम्यूज अस्पताल में विभिन्न स्तर की एण्टी बायोटिक औषधियों का प्रयोग परीक्षण 275 प्रकार के बैक्टीरियाओं से ग्रसित मरीजों पर उलट-पुलट कर किया गया। इन परीक्षाओं में नव-निर्मित डी.एम.सी.टी. इस दृष्टि से अधिक प्रशंसनीय मानी गई कि उसने विषाणुओं का जितना संसार किया उतनी चोट रक्षाणुओं को नहीं पहुंचाई। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्णतया हानि रहित है। इसमें केवल रोग ही नष्ट होते हैं जीवनी शक्ति को क्षति नहीं पहुंचती ऐसा दावा करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं हो सका है।
हल्की खांसी, तीसरे पहर बुखार की हरारत, भूख की कमी, वजन का घटना, रात्रि के अन्तिम पहर में पसीना आना जैसे सामान्य लक्षणों से क्षय रोग की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है। इन चिन्हों के आधार पर यह आशंका की जा सकती है कि हो न हो रोगी पर क्षय का आक्रमण हो चला है।
वस्तुस्थिति का पता तो छाती का स्क्रीनिंग अथवा एक्सरे एवं रक्त, थूक आदि का परीक्षण करने पर ही चलता है। इसके लिए मांस मिनिएचर रेडियोग्राफी (एम.एम.आर.) की सरल परीक्षा पद्धति भी सामने आई है।
आमतौर से क्षय उपचार में लगातार दो-तीन महीने ‘स्टेप्टो माइसिन’ के इन्जेक्शन लगाये जाते हैं एव आइसोनेक्स—पी.ए.एस. जैसी दवाओं का स्थिति के अनुरूप सेवन कराया जाता है।
बचाव उपचार में बी.सी.जी. (वेसीलस काल्मेटेग्वेरिन) के टीके लगाये जाते हैं। यह नामकरण उनके आविष्कर्त्ताओं के नाम पर ही किया गया है। 40 सुइयों की खरोंच वाला यह टीका आरम्भ में बहुत उत्साहवर्धक समझा गया था, पर अब उसकी प्रतिक्रिया संदिग्ध आशंका के रूप में सामने आ रही है। अब क्षय से सुरक्षा प्राप्त करने का यह टीका अमोघ उपचार नहीं रहा वरन् उसके दुष्परिणाम पीछे किसी अन्य व्यथा को साथ लायेंगे ऐसे माना जाने लगा है।
आवश्यक नहीं कि आक्रमण बाहर से ही हों अपनी आन्तरिक दुर्बलता भी गृह युद्ध खड़ा कर देती है। ‘घर का भेदी लंका ढावे’ वाली कहावत भी बहुत बार सामने आती है। अवांछनीय व्यवहार से रुष्ट होकर अपने उपयोगी तत्व विद्रोही बनकर आक्रमणकारी शत्रु का रूप धारण कर लेते हैं और उस अन्तः विस्फोट का स्वरूप भी विप्लवी गृह युद्ध जैसे बन जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए रोगों और विषाणुओं की संख्या भी कम नहीं होती।
जब कारण वश शरीर के कुछेक जीवकोष विद्रोही हो जाते हैं तो सामान्य रीति-नीति की मान-मर्यादा तोड़कर उद्धत उच्छृंखल गतिविधि अपनाकर मनमर्जी की चाल चलते हैं। यह उद्धत विद्रोही ही केन्सर का मूल कारण हैं।
आमतौर से जीवकोष अपनी भूख तथा आवश्यकता तरल रक्त से प्राप्त करते रहते हैं किन्तु जब उनमें से कुछ असन्तुष्ट अपने लिए मनमर्जी का वैभव चाहते हैं तो समीपवर्ती जीवकोषों पर टूट पड़ते और उन्हें लूट-खसोटकर अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हैं इतना ही नहीं वे अपने लिए निर्धारित क्षेत्र और कार्य की मर्यादाओं को तोड़कर रक्त प्रवाह में तैरते हुए किसी भी अंग में जा घुसते हैं और वहां भी कत्लेआम का दृश्य उपस्थित करते हैं। जहां भी उन्हें पैर टिकाने को जगह मिली वहीं के अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं। यही है केन्सर की मूल प्रकृति।
केन्सर को उत्पन्न करने वाले उपकरण ‘कारसिनोज’ कहे जाते हैं। कोलतार, रेडियम, मादक द्रव्य इसी वर्ग में आते हैं। इनका गहरा प्रभाव शरीर पर पड़ेगा तो केन्सर की आशंका बढ़ेगी। अधिक आग तापने अथवा किसी अंग विशेष का अनावश्यक अतिघर्षण होते रहने से भी यह विपत्ति सामने आ खड़ी होती है। रतिक्रिया की सीमा एवं कोमलता का व्यतिक्रम होने से स्त्रियों की जननेन्द्रिय केन्सरग्रस्त हो जाती हैं।
एक ओर विषाणुओं की विभीषिका सामने खड़ी है और रुग्णता से लेकर मरण तक के साज संजो रही है वहां दूसरी ओर जीवन रक्षा की सेना भी कमर कसकर सामने खड़ी है। हमारे शरीर में ही एक विशालकाय महा भारत रचा हुआ है। कौरवों की कितनी ही अक्षौहिणी सेना जहां अपने दर्प से दहाड़ रही है वहां पाण्डवों की छोटी टुकड़ी भी आत्म-रक्षा के लिए प्राण हथेली पर रखकर युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। रक्ताणु हमारी जीवन रक्षा के अदम्य प्रहरी हैं वे विषाणुओं को परास्त करके जीवन सम्पदा को बचाने के लिए कट-कट कर लड़ते हैं अपने प्राण देकर के भी शत्रु का अपनी भूमि पर अधिकार न होने देने का प्रयत्न करते हैं हमारे अन्तः क्षेत्र में, धर्मक्षेत्र में, कर्मक्षेत्र में चलती रहने वाली यह महाभारत जैसी पुण्य प्रक्रिया देखने समझने ही योग्य है।
रक्त को नंगी आंखों से देखें तो वह लाल रंग का गाढ़ा प्रवाही मात्र दिखाई देता है, पर अणुवीक्षण यन्त्र से देखने पर उसमें असंख्य रक्ताणु दिखाई देते हैं। इनकी आकृति-प्रकृति की अब अनेकों जातियां जानी परखी जा चुकी हैं। यह रक्ताणु भी कोशिकाओं की तरह ही जन्मते-मरते रहते हैं। प्रायः उनकी आयु तीन महीने होती है। उनकी बनावट स्पंज सरीखी समझी जा सकती है जिसके रन्ध्रों में ‘हेमोग्लोविन’ नामक रसायन भरा होता है। यह रक्ताणु रक्त के साथ निरन्तर समस्त शरीर में भ्रमण करते रहते हैं और अपने तीन मास के स्वल्प जीवन काल में प्रायः तीन सौ मील का सफर कर लेते हैं।
हेमोग्लोविन कभी रक्त का प्रमुख रसायन माना जाता था। अब उसे चार श्रृंखलाओं में जुड़ा हुआ प्रायः 600 अमीनो अम्लों का समूह पाया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता लाइनस सी. पलिंग ने अपने दो साथियों के साथ इन रक्ताणुओं की शोध में अभिनव जानकारियों की कितनी ही कड़ियां जोड़ी हैं।
कितने ही रोग इन रक्ताणुओं के साथ जुड़े होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। कुछ विशेष कबीलों में कुछ विशेष प्रकार के रक्ताणु पाये जाते हैं तद्नुसार उनकी शारीरिक स्थिति में अमुक रोग का प्रतिरोध करने की—अमुक रोग से आक्रान्त होने की विशेष स्थिति देखी गई है। शारीरिक ही नहीं मानसिक क्षेत्र में भी यह रक्त विशेषता जमी रहती है। कुछ परिवारों के लोग बहुत भोले और डरपोक पाये जाते हैं जबकि किन्हीं वर्गों में आवेश, उत्तेजना और लड़ाकू प्रवृत्ति का बाहुल्य रहता है। राजपूतों की लड़ाकू प्रवृति और जुलाहों का डरपोकपन प्रसिद्ध है। सम्भवतः ऐसी विशेषताएं रक्ताणु की परम्परागत स्थिति के कारण उत्पन्न होती है।
पिछले पन्द्रह वर्षों में तीस से अधिक प्रकार के असामान्य हीमोग्लोबिन वर्गों का पता लगाया जा चुका है। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो. वर्नाव एम. इंग्राम ने इनके वर्गीकरण तथा क्रियाकलापों की गहरी शोध करके यह पाया है कि शरीर एवं मन के रुग्ण एवं स्वस्थ होने में यह रक्त रसायन असाधारण भूमिका सम्पन्न करते हैं। अफ्रीका में कोई 80 हजार बच्चे इन रक्त रसायनों की विकृति के साथ जन्म लेने के कारण स्वल्प काल में ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इसी प्रकार उस महाद्वीप के एक कबीले में ऐसे रक्ताणु पाये गये जो मलेरिया के ‘प्लास्पोडियम फाल्सी पेरम’ कीटाणुओं से शरीर को तनिक भी प्रभावित नहीं होने देते। अन्य कबीलों के लोग उस क्षेत्र में आकर रहे तो तुरन्त मलेरिया ग्रसित हो गये किन्तु वहां के मूल निवासी मुद्दतों से इन्हीं मच्छरों के बीच रहते हुए कभी बीमार नहीं पड़े।
स्वीडन के शरीर विज्ञानी प्रो. फोलिंग इस बात पर जोर देते हैं कि विषाणुओं को मारने के लिए एन्टीवायटिक्स अथवा दूसरी प्रकार की जो मारक औषधियां दी जा रही हैं उनका प्रचलन बन्द किया जाय और स्वस्थ रक्ताओं को अधिक समर्थ बनाने के प्रयोगों को प्राथमिकता दी जाय। रोगों का स्थायी निवारण और सुदृढ़ स्वास्थ्य का संरक्षण इसी नीति को अपनाने से सम्भव होगा।
मारक औषधियां मित्र शत्रु का—अपने पराये का भेद किये बिना अपनी अन्धी तलवार दोनों पक्ष के योद्धाओं को मारने के लिए प्रयुक्त करती हैं। विषाणु मरें, सो ठीक है, पर स्वस्थ कणों की सम्पदा खोकर तो हम इतने दीन-हीन बन जाते हैं कि वह दुर्बलता भी रुग्णता से कम कष्टकारक नहीं होती। उससे भी मन्द गति से दीर्घकाल तक चलती रहने वाली रुग्णता ही जम बैठती है।
प्रकृति ने जीवन की प्रखरता को संजोये रखने के लिए संघर्ष आवश्यक समझा और विषाणुओं, रक्ताओं में निरन्तर संघर्ष होते रहने की व्यवस्था बनादी ताकि हम युद्ध कौशल में प्रवीण होकर सच्चे अर्थों में समर्थ और प्रगतिशील बन सकें।
इस युद्ध से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि शत्रु को मारने से भी अधिक उपयोगिता आत्म-पक्ष को सबल बनाने की है। संसार में फैली हुई अनीति के दमन के लिए आवेश में आकर उपयोगी-अनुपयोगी की परख किये बिना अन्धाधुन्ध तलवार चलना हानिकारक है। लाभ इसमें है कि नीति पक्ष को परिपुष्ट किया जाय जिससे बिना कठिन संघर्ष के ही शत्रु पक्ष परास्त हो सके साथ ही आत्म-पुष्टि से चिरस्थायी स्वास्थ्य सन्तुलन की—शान्ति और प्रगति की अभिवृद्धि हो सके। हमारी जीवन नीति एवं सुधार व्यवस्था का संचालन इसी आधार पर होना चाहिए।
असुरता के संहार में प्रवृत्त—अन्तः चेतना
कैंसर क्रोनिक स्टिमुलश से बढ़ता है, जिसका अधिकांश कारण धूम्रपान (स्मोकिंग) है। क्रोनिक सविसाइटिस (स्त्री-रोग), पेट का फोड़ा (पेष्टिक अल्सर) आदि से भी 5 प्रतिशत कैंसर हो सकता है। पर डाक्टरों की राय में इन सबका कारण अपनी ही चिन्तायें, उतावलापन और मिर्च-मसालों वाला गरिष्ठ आहार होता है। एक बार क्रोनिक स्टिमुलश पैदा हो जाने के बाद वह कोष (सेल्स) को विकृत करना प्रारम्भ करता है। 1 से 2, 2 से 4 इस क्षिप्र गति से बढ़ता हुआ यह रोग सारे शरीर पर उसी तरह छा जाता है जिस तरह दहेज रिश्वत, मिलावट, अन्धविश्वास, अशिक्षा और बाल-विवाह आदि कुरीतियां भारतीय जीवन को आच्छादित किये हैं। यदि प्रारम्भ में ही इसे नष्ट न किया गया तो कैंसर का ठीक होना कठिन हो जाता है।
मनुष्य जीवन की एक विस्तृत प्रक्रिया का नाम समाज है। हम जिस गांव में, मुहल्ले या नगर में रहते हैं—समाज वहीं तक सीमित नहीं। हमारा प्रान्त, हमारा देश, पड़ौसी देश और सारा विश्व एक समाज है। समाज की सीमायें विशाल हैं। अपने आप तक सीमित सुधार की प्रक्रियायें सरल हो सकती हैं किन्तु हम इस व्यापक समाज से इतने प्रभावित और बंधे हुए हैं कि उसकी हर छोटी-बड़ी बुराई से हमारा टकराव हर घड़ी होता रहता है। हमारी सज्जनता, हमारी शुद्धता, हमारा सौष्ठव तभी स्थिर रह सकता है जब सारा विश्व-समाज ही शुद्ध, सज्जन और सौम्य हो। इस जटिल समस्या को हल करना तभी सम्भव है जब विश्व-संस्कृति की सभी भलाई वाली शक्तियां निरन्तर क्रियाशील रहें और बुराइयों पर उसी प्रकार दबाव डालती रहें, जिस तरह शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग, शोक और बीमारियों का संहार औषधियों से करते रहते हैं। जब शरीर में बाहरी कीटाणुओं से या भीतरी किसी कारण से कोई रोग हो जाता है तो एन्टीबायटिक्स दवाइयों द्वारा उस पर सीधा घातक प्रभाव डाला जाता है। यह औषधियां शरीर के सारे रक्त का दौरा करती हैं और जहां कहीं भी रोग-कीटाणुओं को छिपा हुआ पाती हैं, मार गिराती हैं।
कई बार इस संघर्ष में अपनी भी हानि होती है। औषधि शास्त्र कहता है—यदि 100 शत्रु नष्ट करने में एक अपना भी मारा जाये तो कुछ हर्ज नहीं, पर सीधे मुकाबले का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। पेट में कई बार राउन्ड बाल्व्स पैदा हो जाते हैं। यह परजीवी (पैरासाइट) कीड़े (बैक्टीरिया) आंतों को उस तरह खाने लगते हैं जैसे फैशनपरस्ती, नशे-बाजी वासनायें स्वास्थ्य को खाने लगती हैं। इस स्थिति में डॉक्टर कोई दस्तावर औषधि देते हैं और रक्त में होने वाले विषैले प्रभाव से शरीर को बचाते हैं। इन औषधियों में तीव्रता होती है, वह पेट की सारी गन्दगी झाड़ फेंकती हैं। यह क्रिया कुछ तीव्र होती है, इससे पाचन वाले अम्ल (एसिड्स) भी पटक जाते हैं पर उनका चला जाना भी रोग के आक्रमण से हो जाने वाली हानि की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है। इसीलिये सीधे संघर्ष में कुछ लोगों को शारीरिक या मानसिक कष्ट भी हो, तो भी प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिए।
कई बार डॉक्टर उचित इलाज का पता नहीं लगा पाते, तब वे प्रभावित अंग से रोग के कीटाणु निकाल कर उन्हें कल्चर प्लेट पर रखते हैं और उन पर कई एन्टी बायोटिक्स औषधियों की एक-एक बूंद रखते जाते हैं। जो औषधि अधिक कीटाणुनाशक हुई, बाद में उसी का प्रयोग किया जाता है। बुराइयों से सतर्कता तो प्रत्येक स्थिति में रखनी ही चाहिए अन्यथा पता न चलेगा और वह भीतर ही भीतर हमें नष्ट कर दें सकती है। शराब पीने वालों में चर्बी की एक सतह जिगर के कोषों के ऊपर जम जाती है। उससे जिगर के कोषों को खाद्य (ऑक्सीजन) मिलना बन्द हो जाता है। शराब पीने वाले को पता नहीं चलता और भीतर-ही-भीतर सिरोसिस आफ लिवर बीमारी हो जाती है। मनुष्य को अपने स्वभाव, समाज की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। यदि ऐसा न हुआ और बीमारी पककर फूटी तो उसका संभालना कठिन हो जाता है।
डॉक्टर और स्वास्थ्य-विशेषज्ञ जानते हैं कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं—(1) एयरोबिक अर्थात् जिन्हें जिन्दा रहने के लिये ऑक्सीजन आवश्यक है। (2) एन एयरोबिक अर्थात् जिन्हें आवश्यक नहीं। कोई अंग सड़ जावे (ग्रैगीन) क्लास्टेडियम बेसलाई, क्लास्टेडियम एडेमेन्टीस एवम क्लास्टेडिक सेप्टिकी जो एन एयरोबिक हैं उनको मारने के लिये एयरोबिक वातावरण पैदा करना आवश्यक है।
बुराई न बढ़े, उसके लिये यह भी आवश्यक है कि उन्हें पोषण न मिले। गुण्डा तत्वों से डरकर लोग चाहते हुए भी उन्हीं का समर्थन और हां में हां मिलाने लगते हैं। इससे उनका कुनबा और भी फलने-फूलने लगता है। यदि लोग उनका समर्थन और पोषण बन्द कर दें तो वह अपने आप मरकर नष्ट हो जायें।
टी.बी. के कीटाणु इसी सिद्धांत पर मारे जाते हैं। यह एसिड फास्ट बेसिलाई [जो एसिड से भी नहीं मरते] हैं। जब इस तरह के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब डॉक्टर स्ट्रप्टोमाइसीन देते हैं। यह टी.बी. के कीटाणु की ऊपरी झिल्ली [लायपाइड कवरिंग] पर चारों ओर से घेरा डाल लेता है। इससे उस कीटाणु की मुसीबत आ जाती है। दुष्ट अपना खाद्य भी नहीं ले सकता और भीतर घुटकर मर जाता है। जो बुराइयां सीधी टक्कर से नहीं जीती जा सकतीं, उनको पोषण न मिले तो वे टी.बी. के कीटाणु की तरह आप नष्ट हो जाती हैं।
जहां इस स्थिति में भी काम न बने वहां भलाई की शक्ति का उद्बोधन करना और उसे मुकाबले के लिये ललकारना आवश्यक हो जाता है। नान स्पेसिफिक थैरेपी के अन्तर्गत कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो लगातार औषधि-सेवन से भी अच्छी नहीं होती। उदाहरण के लिये चमड़ी की बीमारी—एक्जिमा। उस स्थिति में डॉक्टर मुकाबले की शक्ति तैयार करते हैं। रोगी के शरीर का 5 सी.सी. शुद्ध रक्त लेकर रोगी के शरीर में प्रवेश [इन्जेक्ट] कर दिया जाता है। यह प्रोटीन होता है और भीतर शरीर में पहले से ही प्रोटीन होता है। जब तक अच्छाई बुराई में भेद न किया गया था, बुराई भी दहेज, पर्दा प्रथा, नशा आदि की तरह साथ-साथ पल रही थी। पर जब कुछ यज्ञ, हवन, जप, तप, बिना दहेज विवाह, नशा—उन्मूलन आदि की स्थिति बनी तो दूसरे लोगों ने भी अनुभव किया कि बुराई वह है जो अपनी या समाज के किसी भी वर्ग का अहित करती है भले ही वह कोई परम्परा बन गई हो। जब इस तरह का विवेक जाग पड़ता है तो अपनी बुराइयों का उन्मूलन ठीक ऐसे ही सरल हो जाता है, जैसे एक्जिमा में रोगी का ही रक्त इन्जेक्शन कर देना। भीतर वाले प्रोटोन उन्हें बाहरी समझ कर हमले के लिए तैयार होते हैं पर जब वे अनुभव करते हैं कि अरे! यह तो अपने ही बन्धु और हितैषी हैं तब उनसे मिल जाते हैं और एक नई शक्ति अनुभव करते हैं। अब सब मिलकर एक्जिमा के विरोध में लड़ पड़ते हैं और उस न मिटती जान पड़ने वाली बीमारी को भी नष्ट कर डालते हैं। अच्छाई को उकसाकर बुराई को नष्ट करने का प्रयोग बहुत ही उपयोगी और सफल सिद्ध होता रहा है।
यह वैज्ञानिक प्रयोग हैं जिनसे शरीर के समान ही अपने को शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। उसी के आधार पर सुख, समृद्धि और विश्वशान्ति का वातावरण पैदा किया जा सकता है।
सल्यूलोग आवरण से आच्छादित तरल प्रोटोप्लाज्मा से बने जीवाणु किसी भी स्थान पर नमी, आदि पाकर स्वयं ही जन्म ले लेते हैं यह इतनी सूक्ष्म सत्ता है कि एक इंच की लम्बी लकीर में इन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाये तो 25000 जीवाणु बड़े मजे में खड़े हो जायेंगे। इतनी आदमी एक पंक्ति में खड़े किये जायें और यह माना जाये कि एक व्यक्ति औसतन 1 फुट जगह लेगा तो कुल आदमियों के लिए 5 मील लम्बी सड़क आवश्यक होगी। देवत्व सूक्ष्म तत्व है अनुभूति के लिए वैसी ही सूक्ष्म बुद्धि दूरदर्शी समीक्षा चाहता है यह न हो तो मनुष्य सामान्य स्वार्थ को ही उस श्रेणी में मानकर उसके लाभों से वंचित हो सकता है।
विषाणु तो उससे भी सूक्ष्म और प्रभावी सत्ता है एक इंच में यह 141000 आसानी से बैठ सकते हैं—अर्थात् यदि वह आदमी बराबर हों और यह माना जाये कि उनमें से प्रत्येक को 1 फुट ही जगह चाहिए तो 26 मील सड़क की आवश्यकता होगी। तात्पर्य यह हुआ कि बुराई की शक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है। वह अब आ धमके यह पता लगाना भी कठिन है जब तक कि उतनी ही पैनी और सूक्ष्म निरीक्षण बुद्धि न रखें।
जीवाणु जल में भी होते हैं और इस रूप में वे लोकसेवी हमारे जीवन के पोषक के रूप में काम करते हैं। मिट्टी में पड़े मल और सड़न को बैक्टीरिया ही खाकर उसे अच्छी मिट्टी में बदलते रहते हैं। देव-प्रवृत्तियां भी इसी तरह अपने को बढ़ाने में सहायक होती हैं। साथ ही वह सृष्टि के उच्छिष्ट तत्व सड़ाकर सब को नष्टकर स्वच्छ, पवित्र वातावरण बनाती है। जिससे सर्वत्र सुख-शान्ति और प्रसन्नता बढ़ती है। जीवाणु 10 या 20 मिनट में ही अन्य जीवाणुओं को जन्म देने लगते हैं और 24 घण्टे में 17000000 जीवाणुओं में परिणत हो जाते हैं। देवत्व एक क्षण के लिए भी उदित हो तो दूरगामी शान्ति और व्यवस्था की नींव गहरी जमा जाता है।
दूसरी ओर विषाणु है जो जीवाणु के ही पैरों में लगा चला आता है। बुराइयां सदैव छद्म वेष में देवत्व के बाने में आती हैं अन्यथा उन्हें स्थान ही न मिले इसलिए अच्छाइयां जहां हमारे जीवन को अभीष्ट हैं। वहीं सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अतिथि और मित्र बनकर आये परिजनों में ही कहीं कोई अपनी द्विविधा और भ्रम का लाभ उठाकर कोई चोर उचक्का तो नहीं आ धमकता।
दूध में पड़ा बैक्टीरिया उसे दही बना देता है देवत्व और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति समाज को भी उसी तरह सुन्दर बना देती है, जैसे दूध की अपेक्षा दही अधिक सुपाच्य हो जाता है। अपने जीवन में छोटी से छोटी वस्तु का उपयोग है। यदि हम भलाई के हर कण को अपनाने की कला सीख जायें तो हर किसी के आदर और विश्वास के पात्र बन सकते हैं, पर विषाणु जहां भी पहुंच जायें वहीं बीमारी पैदा कर दें अर्थात् बुराई के कर्म ही नहीं विचार भी हमारे पतन का आधार बन जाते हैं।
जीवाणु तथा विषाणु दोनों की ही संचार और विस्तार व्यवस्था बड़ी व्यापक है, पक्षियों के परों में लिपटे जहाजों में चढ़ कर यात्रियों के माध्यम से भी ये एक स्थान-से एक देश से, दूसरे स्थान-दूसरे देश पहुंच जाते हैं। और सर्वत्र महामारी की स्थिति पैदा कर देते हैं कुछ न मिले तो हवा ही उनके लिए उपयुक्त वाहन है। इसी से यह कहीं भी जा पहुंचते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों का क्षेत्र भी उसी तरह सर्वत्र खुला पड़ा है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अर्वाचीन युग के देवत्व की भी अपने वर्तमान जीवन में बुला सकते हैं और नाटकों, फिल्मों से भी अच्छे बनने की प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरों के अच्छे आचरण हमारे जीवन दीप बन सकते हैं। और उनकी शिक्षायें भी वही प्रेरणा दें सकती हैं। बुराइयों के लिए भी ठीक यही स्थिति है बुलायें तो मन ही मन से करोड़ों मनोविकार आमन्त्रित करलें दृढ़ता हो तो दृष्टि में पड़ने वाली कुत्सा भी अन्दर झांकने न पाये।
हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्तियां जड़ न जमा पायें उसके लिए उन्हें मारने की मुहीम जाग्रत रखनी चाहिए। एण्टी बायटिक औषधियां जिस तरह शरीर में पहुंच कर वहां के विषाणुओं को चारों ओर से घेर कर रसद मार्ग काट कर उन्हें आत्मघात को विवश करती हैं, उसी तरह आत्म सुधार के लिए हमें प्रलोभनों को मार भागने का—बुराइयों से लड़ने का माद्दा अपने अन्दर से ही पैदा करना चाहिए। यदि ऐसा करलें तो वह हमारी उसी तरह हानि नहीं कर सकतीं जिस तरह हास्पिटलों में टी.बी., कैन्सर आदि के मरीज भरे पड़े रहते हैं। स्वाभाविक है कि वहां विषाणुओं का सरोवर लहरा रहा हो किन्तु उसी वातावरण में डॉक्टर लोग दिन-दिन भर काम करते रहते हैं। फिर भी उनका रत्ती भर भी अहित नहीं हो पाता।
दैवी अंश प्रबल हों तो वह सशक्त जीवाणुओं की तरह शरीर की ढाल का कार्य करते हैं। उससे असुरता हावी नहीं होने पाती, आत्म सुधार की सबसे अच्छी प्रक्रिया यह है कि हम निरन्तर रचनात्मक विचारों को मस्तिष्क में विकसायें, रचनात्मक कार्य करते रहें उससे बुराइयां अपने आप ही झांक कर लौट जाती हैं। जिस घर में पहले ही समर्थ लोग रहते हों वहां चोर उचक्के झांक कर ही लौट जाते हैं।
लेकिन यदि सीलन, सड़न, गलन अपने भीतर ही हो तो कमजोर भले मानस को भी सशक्त बदमाशों द्वारा सताये जाने की तरह बुराइयों को पनपने का भीतर ही आधार मिल जायेगा। बाहर के विषाणु शरीर में आयें पर शरीर सशक्त हो, पाचन यन्त्र ठीक काम करते हों, रुधिर में श्वेताणुओं की कमी न हो तो विषाणु रत्ती भर असर नहीं डाल पायेंगे उल्टे नष्ट हो जायेंगे पर भीतर विजातीय द्रव्य भरा हो, आदमी में आकर्षणों की सड़न भीतर-भीतर बुश रही हो तब तो वे अपनी शक्ति भीतर ही बढ़ा कर हमारे विनाश का कारण बन जायेंगे यहीं नहीं विजातीय द्रव्य के बाद वे शरीर की कोशाओं को भी खाने लगेंगे तब फिर जीवन का अन्त होगा ही।
प्रकाश में विषाणुओं को मार देने की शक्ति है। हमारे जीवन में प्रकाश तत्व बना रहे—विवेक बना रहे तो न केवल भलाई की शक्ति—देवत्व का विकास और उसके फलितार्थों से लाभान्वित होते रह सकते हैं। आसुरी तत्व वे चाहे कितने ही अदृश्य और शक्ति शाली क्यों न हों जानकारी में आते रहें और उन्हें नष्ट करने मार कर भगा देने का साहस हमारे जीवन में बना रहना चाहिए।
प्राणी यों प्रकृति की विपरीत चपेट में आकर अक्सर अस्तित्व गंवा बैठता है। नियति के उग्र परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाता और विपरीत परिस्थिति के सामने अपने को निरीह असमर्थ अनुभव करता है, पर ऐसा तभी होता है जब वह उस आपत्ति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार न हो। यदि प्राणी को विपरीत अनभ्यस्त परिस्थिति में रहने को विवश होना पड़े तो वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए क्रमशः ऐसे परिवर्तन उत्पन्न कर लेता है—ऐसी विशेषता का उत्पादन कर लेता है जिसके आधार पर वह प्राणघातक समझी जाने वाली परिस्थितियों से भी तालमेल बिठा ले और अपना अस्तित्व कायम रख सके, सुविधा पूर्वक निर्वाह कर सके।
जीवाणुओं की असह्य तापमान पर मृत्यु हो जाती है। वे अधिक उष्णता एवं शीतलता सहन नहीं कर सकते, यह मान्यता अब पुरानी पड़ चली है। पानी खौलने से अधिक गर्मी और 270 आ. से. नीचे शीत पर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाने की बात ही अब तक समझी जाती रही है। इसका कारण यह था कि शरीर में पाया जाने वाला ग्लिसरोद रसायन असह्य तापमान पर नष्ट हो जाता है और जीवाणु दम तोड़ देते हैं अब वे उपाय ढूंढ़ निकाले गये हैं कि इस रसायन को ताप की न्यूनाधिकता होने पर भी बचाया जा सके और जीवन को अक्षुण्ण रखा जा सके।
अत्यधिक और असह्य शीतल जल में भी कई प्रकार के जीवित प्राणी निर्वाह करते पाये गये हैं इनमें से प्रोटो—जुआ, निमैटौड, क्रस्टेशिया, मोलस्का आदि प्रमुख हैं। येलोस्टोन की प्रयोगशाला में लुइब्राक और टामस नामक दो सूक्ष्म जीव-विज्ञानी—माइक्रो वायोलाजिस्ट यह पता लगाने में निरत हैं कि जीव सत्ता के कितने न्यून और कितने अधिक तापमान पर सुरक्षित रह सकने की सम्भावना है। वे यह सोचते हैं कि जब पृथ्वी अत्यधिक उष्ण थी तब भी उस पर जीवन सत्ता मौजूद थी। क्रमश ठण्डक बढ़ते जाने से उस सत्ता ने क्रमिक विकास विस्तार किया है, पर इससे क्या—अति प्राचीन काल में जब जीवन सत्ता थी ही तो वह विकसित अथवा अविकसित स्थिति में अपनी हलचलें चला ही रही होगी भले ही वह अब की स्थिति की तुलना में भिन्न प्रकार की अथवा पिछड़े स्तर की ही क्यों न रही हो। विकसित प्राणी के लिए जो तापमान असह्य है वह अविकसित समझी जाने वाली स्थिति में काम चलाऊ भी हो सकता है।
यदि यही तथ्य हो तो फिर जीवन की मूल मात्रा को शीत, ताप के बन्धनों से युक्त माना जा सकता है और गीताकार के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मा को न आग जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न जल डुबा सकता है। पंचभूतों की प्रत्येक चुनौती का सामना करते हुए वह अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकने में पूर्णतया समर्थ है।
समुद्र तट के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली धूसर रंग की मक्खी ‘एफिड्रिल को 45 डिग्री से 51 डिग्री से. के बीच तापमान वाले गर्म जल में प्रवेश करते देखा गया है। यह प्राणियों के जीवित रहने को असम्भव बनाने वाले गर्मी है। सामान्यतया धरती की सतह पर 21. से. तापमान रहता है। प्राणियों को उतना ही सहन करने का अभ्यास होता है। अधिक उष्ण या अधिक ताप के वातावरण में रहने वाले जन्तुओं को विशिष्ठ स्थिति के अभ्यस्त ही कह सकते हैं।
एफिड्रिड मक्खी के अतिरिक्त कुछ जाति के बैक्टीरिया भी ऐसे पाये गये हैं जो खौलते पानी के 92 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान में भी मजे से जीवित रहते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित गर्म जल के झरने प्रायः इसी तापमान के हैं और उनमें जीवित बैक्टीरिया पाये गये हैं। इन गर्म झरनों अथवा कुण्डों में एक प्रकार की काई सी मोटी परत जमी रहती है जिसे हिन्दी में शैवाल कहा जाता है अंग्रेजी में उसका नाम एल्गी है। इसमें जीवन रहता है। आमतौर से वह 75 डिग्री से. तक गर्म जल में मजे का निर्वाह करती है बैक्टीरिया उसी के सहारे पलते हैं। एफिडिड मक्खी के, प्रमुख भोजन यह एल्गी ही है उस प्राप्त करने के लिए वह उस असह्य तापमान के जल में डुबकी लगाती है और बिना जले, झुलसे अपना आहार उपलब्ध करती है।
यह तो हुई छोटे जीवों की बात, अब अधिक कोमल समझे जाने वाले मनुष्यों की बात आती है वह भी प्रकृति की असह्य कही जाने वाली स्थिति में निर्वाह करने के लिए अपने को ढाल सकता है। उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहने वाले एक्सिमो लोग अत्यधिक शीत भरे तापमान में रहते हैं। भालू, हिरन और कुत्ते भी उस क्षेत्र में निवास करते हैं। वनस्पतियां और वृक्ष न होने पर पेट भरने के लिए मांस प्राप्त कर लेते हैं इसके लिए उसने बर्फ की मोटी परतें तोड़ कर नीचे बहने वाले समुद्र में से मछली पकड़ने की अद्भुत कला सीखली है आयुध साधन रहित होते हुए भी हिरन, भालू और कुत्तों का भी वे शिकार करना सीख गये हैं और लाखों वर्ष से उस क्षेत्र में निर्वाह कर रहे हैं।
प्रकृति के अनोखे वरदान
पैस्फिक सागर में गोता लगाकर मोती ढूंढ़ने वालों को पता चला कि ‘‘स्टार फिश’’ (यह तारे की तरह चमकने वाली छोटी सी मछली होती है) ही अधिकांश सीपियों को नष्ट कर डालती है अतएव वे मोती ढूंढ़ने से पहले इन स्टारफिशों को ही समूल नष्ट कर डालने के लिये जुट पड़े। उन्होंने इन्हें पकड़ पकड़ कर काटना शुरू कर दिया। एक, दो, दस, पचास, सैकड़ा हजार—कितनी ही स्टारफिशें काट डाली गईं पर रावण के मायावी सिरों की भांति वे कम न हुईं उलटे उनकी संख्या बढ़ती ही गई। अभी तक तो उनकी उपस्थिति ही चिन्ताजनक थी अब तो उनकी आश्चर्यजनक वृद्धि और भी कष्टदायक हो गई अन्त में यह जानने का फैसला किया गया कि आखिर यह स्टारफिशों की वृद्धि का रहस्य क्या है?
सावधानी से देखने पर पता चला कि जो स्टारफिश काट डाले गये थे उनका प्रत्येक टुकड़ा स्टारफिश बन चुका था अभी तक अमीबा, हाइड्रा जैसे एक कोशीय जीवों के बारे में ही यह था कि ये अपना ‘‘प्रोटोप्लाज्म’’ दो हिस्सों, दो से चार चार से आठ हिस्सों में बांटकर वंश वृद्धि करते जाते हैं पर अब इस बहुकोशीय जीव को काट देने पर भी जब एक स्वतंत्र अस्तित्व पकड़ते देखा गया तो जीव शास्त्रियों का प्रकृति के इस विलक्षण रहस्य की ओर ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। तब से निरन्तर शोध-कार्य चलता रहा। और देखा गया कि नेस सलामैसीना, आइस्टर, स्नेल (घोंघा फ्रेश वाटर मसल (शम्बूक) साइलिस, चैटोगैस्टर स्लग मन्थर) पाइनोगोनाइड (समुद्री मकड़ी) आदि कृमियों में भी यह गुण होता है कि उनके शरीर का कोई अंग टूट जाने पर हो नहीं वरन् मार दिये जाने पर भी वह अंग या पूरा शरीर उसी प्रोटोप्लाज्म से फिर नया तैयार कर लेते हैं। केकड़ा तो इन सबमें विचित्र है। टैंक की सी आकृति वाले इस जीव की विशेष यह है कि अपने किसी भी टूटे हुए अंग को तुरन्त तैयार कर लेने की प्रकृति दत्त सामर्थ्य रखता है।
यह तथ्य जहां इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इच्छा शक्ति पदार्थ का बन्धन रहित उपयोग कर सकने में समर्थ है वहां इस बात को भी प्रमाणित कर रहे हैं कि आत्म चेतना एक शक्ति है और वह भौतिक शक्तियों से बिलकुल भिन्न मरण-धर्म से विपरीत है। उस पर जरा, मृत्यु आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्म तत्व भले ही वह किसी भी घृणित और तुच्छ से तुच्छ वासना एवं इच्छा शक्ति के रूप में क्यों न हो, इतना सशक्त है कि स्वेच्छा से न केवल अपने भीतर से उत्पादन की क्रिया आप ही करता रहता है वरन् अपने पूर्णतया मुर्दा शरीर को भी बार-बार जीवित और नया कर सकता है। इन महान आश्चर्यों को देखकर ही लगता है भारतीय तत्व:दर्शियों ने सृष्टि विकास क्रम को ईश्वर इच्छा शक्ति पर आधारित माना। इसी आधार पर विकासवाद जैसा सिद्धान्त विखण्डित हो जाता है। जब प्रकृति के नन्हे-नन्हे जीवन, उत्पादन, उत्पत्ति और विकास की क्रिया में समर्थ होते हैं तो कोई एक ऐसा विज्ञान भी हो सकता है जब कोई एक स्वतन्त्र इच्छा शक्ति अपने आप पंच महाभूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश) के संयोग से अपने आपको प्रकट कर दें यों देखने में यह क्रिया बीज और वंशानुगत होती प्रतीत होती है।
हाइड्रा देखने में ऐसा लगता है जैसे एक स्थान पर फूल-पत्ते इकट्ठा हों। उसके अंग की कोई एक पंखुड़ी एक ओर बढ़ना प्रारम्भ होती है और स्वाभाविक वृद्धि से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह अधिक बढ़ा अंग अपने आपको मूल भाग से अलग कर लेता है और वह एक स्वतन्त्र अस्तित्व बन जाता है। पैरामीशियम, यूग्लीना आदि एक कोशीय जीवों में प्रजनन का यही नियम है जो यह बताता है कि आत्म-सत्ता को एक सर्वांगपूर्ण शरीर यन्त्र के निर्माण के लिये करोड़ों वर्षों के विकासक्रम की आवश्यकता या प्रतिबन्ध नहीं हैं यदि उसे अपने लघुत्तम या परमाणिविक स्वरूप का पूर्ण अन्तःज्ञान हो जाय तो वह कहीं भी कैसा भी रूप धारण करने में समर्थ हो सकता है। सम्भवतः अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा यह सिद्धियां इसी तथ्य पर आधारित हैं। एक दिन विज्ञान भी इस दिशा में सफल हो सकता है, वह स्थिति आ सकती है, जब सम्मोहन शक्ति के द्वारा रासायनिक ढंग से उत्पादित प्रोटोप्लाज्मा में जीवन उत्पन्न किया जा सके। कैसा भी हो इस महान् उपलब्धि के लिये विज्ञान को पदार्थ तक ही सीमित न रहकर ‘‘भाव’’ को भी संयुक्त करना ही पड़ेगा जैसा कि भारतीय तत्व वेत्ताओं ने अब से हजारों वर्ष पूर्व कर लिया था।
स्टेन्टर अपने प्रोटोप्लाज्मा का 1/60 अंश बाहर का देता है और उसी से एक नया स्टेन्टर तैयार कर देता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा को नयी सन्तान पैदा करने के लिये अपने शरीर का कुल 1/300 वां हिस्सा पर्याप्त है।
प्राणों को जिस प्रतिभा का लाभ मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के रूप में मिला, सृष्टि के अन्य प्राणी भी उस प्राण की महत्ता से सृष्टि के नन्हें-नन्हें जीव भी अनभिज्ञ नहीं। बेशक वह प्राणों के स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकते, प्राणों का असीमित विकास और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली तेजस्विता, दीर्घजीवन प्रज्ञा बुद्धि का लाभ नहीं ले सकते पर उनमें भी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि वे अपने मृत शरीर का बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। परकाया प्रवेश की क्षमता भारतीय योगी ही अर्जित कर सके हैं पर प्रकृति में ऐसे अनेकों योनी हैं जो अपने ही मरे, कुचले टूटे फूटे शरीर का अपने प्राणों के बल पर पुनः उपयोग कर लेते हैं।
जीवित स्पंज को लेकर टुकड़े-टुकड़े कर डालिये, उससे भी मन न भरे तो उन्हें पीसकर पीसकर कपड़े से छान लीजिये। पिसे और कूट कपड़छन किये शारीरिक द्रव्य को पानी में डाल दीजिये। शरीर के सभी कोश धीरे-धीरे फिर एक स्थान पर मिल जायेंगे और कुछ दिन बाद पूरा नया स्पंज फिर से अपनी जीवन यात्रा प्रारम्भ कर देगा। चुनौती है स्पंज की कि जब तक प्राण हैं तब तक मुझे शरीर के अवसान की कोई चिन्ता नहीं। मरना जीना तो मात्र प्राणों का ही खेल है।
हाइड़ा, स्टेन्टर तथा प्लेनेरिया आदि जीवों में यह गुण होता है कि वे अपने शरीर के एक छोटे से अंश को (300 वें भाग तक छोटे टुकड़े को) ही तोड़कर नया शरीर बना देते हैं उन्हें गर्भ धारण भ्रूण-विकास और प्रजनन जैसी परेशानियां उठानी नहीं पड़तीं। लगता है प्राण-तत्व की जानकारी होने के कारण ही प्राचीन भारत के तत्वदर्शी एक भ्रूण से 100 कौरव, घड़े से कुंभज और जघा से सरस्वती पैदा कर दिया करते थे। अन्य एक कोशीय जीवों में पैरामीशियम तथा यूग्लीना में भी एक कोश से विभक्त होकर दूसरा स्वस्थ कोश अर्थात् नया जीव पैदा कर देने की क्षमता होती है। यह घटनायें इस बात की साक्षी भी हैं कि ऐसी क्षमतायें अणु जैसी सूक्ष्म मनःस्थिति तक पहुंचने वाली क्षमता से ही प्रादुर्भूत हो सकती है।
टूटे हुए शारीरिक अंगों के स्थान पर नये अंग पैदा कर लेने की क्षमता ही कुछ कम विलक्षण नहीं ट्राइटन सलामाण्डर, गोह अपने कटे हुए शरीर को क्षति पूर्ति तुरन्त नये अंग के विकास रूप में कर लेते हैं। अमेरिका, अफ्रीका में पाये जाने वाला शीशे का सांप जरा-सा छूने से टूट जाता है पर उसमें यह भी विशेषता होती है कि अपने टूटे हुये अंग को पुनः जोड़ लेता है। आइस्टर, शम्बूक घोंघा, समुद्री मकड़ी, मन्थर आदि जीवों में भी यह गुण होते हैं। स्टारफिश के पेट में कोई जहरीला कीड़ा चला जाये तो वह अपना पूरा पेट ही बाहर निकाल कर फेंक देती है और नया पाचन संस्थान तैयार कर लेती है सलामेसिनानेस, साहलिस तथा काटो मास्टर जीव तो स्पंज की तरह होते हैं उन्हें कितना ही मार डालिये, मरना उनके लिये जबर्दस्ती प्राण निकाल देने के समान होता है जहां दबाव समाप्त हुआ यह अपने प्राणों को फिर मरे मराये शरीर में प्रवेश करके जीवन यात्रा प्रारम्भ कर देते हैं।
जीवन यात्रा में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के लिए भी प्रकृति ने मनुष्य देह में समुचित प्रबन्ध कर रखा है। मनुष्य जो कुछ खाता-पीता है उससे जीवनी शक्ति को उसकी सहायता के लिये कार्बोहाइड्रेट, (कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन) चर्बी, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज द्रव्य मिलते हैं। भोजन में से यह आवश्यक तत्व ग्रहण करने के लिये गले की नली से लेकर आमाशय की छोटी आंतों तक ही पूरी मशीन दिन-रात काम करती रहती है। उससे भी अधिक ध्यान और मशीनरी का निर्माण शरीर में इसके लिये किया गया है कि शरीर द्वारा उत्पन्न होने वाली गन्दगी शरीर से अलग होती रहे। भोजन और शक्ति के अभाव में मनुष्य कुछ दिन जी भी सकता है पर स्वच्छता और सफाई के अभाव में मनुष्य शरीर अधिक दिन तक टिक नहीं सकता।
शरीर के वृक्क प्रतिदिन डेढ़ सेर मूत्र निकालते हैं। इसके द्वारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रीटीनाइन, एमोनिया, सोडियमक्लोराइड, फास्फोरिक अम्ल, मैगनीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की बहुत सी गन्दगी शरीर से बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत प्रतिदिन ढेरों मल निकालती रहती है। शरीर की त्वचा में लाखों की संख्या में ग्रन्थियां होती हैं जो रक्त से पसीने को छान कर बाहर निकालती रहती हैं। हथेली के एक वर्ग इन्च में ही ऐसी कम से कम 3600 ग्रन्थियां होती हैं इससे पता चलता है कि प्रकृति ने शरीर में सफाई की व्यवस्था को सबसे अधिक ध्यान देकर सावधानी से जमाया है यदि शुद्धीकरण की यह क्रिया एक दिन को भी बन्द हो जाये तो शरीर सड़ने लगे और मस्तिष्क पागल हो जाये।
शरीर ही नहीं प्रकृति का हर कण और प्रत्येक क्षण दोष दूषणों के प्रति सजग और सावधान रहता है जहां भी कहीं गन्दगी दिखाई दी प्रकृति उस पर टूट पड़ती है और देखते-देखते गन्दगी को साफ करके उस स्थान को शुद्ध और उपयोगी बना देती है।
जिसे हम नगण्य समझते हैं—उस मिट्टी में भी फफूंद (फगाई) एक्टीनो माइसिटीज तथा दूसरे कई महत्वपूर्ण जीवाणु (बैक्टीरिया) पाये जाते हैं। यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें शक्तिशाली खुर्दबीनों माइस्कोप से ही देखा जा सकता है। पर उनकी इस लघुता में वह महानता छिपी है जो सारे मनुष्य समाज के हितों की रक्षा करती है यदि यह जीवाणु न होते यह सारी पृथ्वी 7 दिन के अन्दर पूरी तरह से मल से आच्छादित हो जाती और तब मनुष्य का जीवित रहना भी असम्भव हो जाता।
जैसे ही कोई सड़ी-गली वस्तु, मल या कोई गन्दगी जमीन में गिरी यह जीवाणु दौड़ पड़ते हैं और इन गन्दगी के अणुओं की तोड़-फोड़ प्रारम्भ कर देते हैं। दूसरे दिन हम उधर जाते हैं तो मल के ढेर के स्थान पर मिट्टी का-सा ढेर दिखाई देता है। लोग उपेक्षा से देखकर निकल जाते हैं पर वहां प्रकृति का एक बड़ा उपयोगी सिद्धान्त काम करता रहता है। यह जीवाणु इस गन्दगी के एक-एक अणु को तब तक तोड़ते फोड़ते रहते हैं जब तक वह सारी की सारी मिट्टी में बदल नहीं जाती।
प्रतिरोध की स्वयं समर्थ शक्ति
सरल और सहज जीने की चाह तो हर किसी को रहती है पर उसकी पूर्ति होना शक्य नहीं। प्रकृति चाहती है कि हर प्राणी को—संघर्ष की पाठशाला में पढ़कर शौर्य साहस की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। सरल जीवन में सुविधा तो है, पर हानि यह है कि प्राणी की प्रखरता नष्ट हो जाती है उसकी प्रतिभा अविकसित रह जाती है। प्रतिकूलता से जूझे बिना जीवन के शस्त्र पर धार नहीं धरी जा सकती, चमक और पैनापन लाने के लिए उसे पत्थर पर घिसा ही जाता है। मनुष्य समर्थ, सबल और प्रखर बना रहे इसके लिए संघर्ष रत रखने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। इसी व्यवस्था क्रम में एक भयंकर लगने वाली रोग कीटाणु संरचना भी है जो जीवन को मृत्यु में बदलने के लिए निरन्तर चुनौती देती रहती है।
आंखों से न दीख पड़ने वाले अत्यन्त सूक्ष्म रोग कीटाणु हवा में घूमते रहते हैं—प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के सहारे रेंगते रहते हैं और अवसर पाते ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी वंश वृद्धि आश्चर्यजनक गति से होती है। उनकी विषाक्तता एवं मारक शक्ति भी अद्भुत होती है। शरीर में सांस, जल या दूसरे किन्हीं आधारों पर वे प्रवेश कर जाते हैं और वहां पहुंच कर अपनी गति-विधियों से भयानक रोगों का सृजन करते हैं। उनके प्रतिरोध को प्रकृति ने व्यवस्था की है। रक्त में पाये जाने वाले श्वेत कीटाणु इन शत्रुओं से जूझते हैं। शरीर की गर्मी तथा विभिन्न स्थानों से निकलने वाले स्राव उन्हें मारते हैं। इस युद्ध में बहुधा मनुष्य की जीवनी शक्ति ही विजयी होती है तभी तो स्वास्थ्य रक्षा सम्भव होती है अन्यथा इन विषाणुओं के द्वारा होते रहने वाले अनवरत आक्रमण से शरीर का एक दिन भी जीवित रह सकना सम्भव न हो सके।
इन रोग कीटाणुओं की असंख्य जातियां हैं और उनके क्रिया-कलाप भी अद्भुत हैं। वर्तमान रोग परीक्षापद्धति में यह पता लगाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया है कि रोगी के शरीर में किन रोग कीटाणुओं का आधिपत्य है। मल-मूत्र, कफ, रक्त आदि की परख करके इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और तद्नुरूप उन्हें मारने की विशेषताओं वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। विषाणुओं की अनेक जातीय के अनुरूप ही उनकी मारक औषधियां ढूंढ़ी गई हैं। इन्हें एंटी बाइटिक्स कहते हैं। इन दिनों इन औषधियों का निर्माण और उपयोग खूब हो रहा है। रोग निवारण का इन दिनों यह प्रमुख आधार है।
पैनसिलीन स्ट्रेप्टोमायसिन वर्ग की रोग कीटनाशक एन्टी बायोटिक्स औषधियों में अब एक और चमत्कारी चरण जुड़ गया है वह है लैडरली लैवोरेटरी द्वारा प्रस्तुत किया गया रसायन डी. एम-सी. टी.। इसका पूरा नाम है—डिमिथाइल क्लोर टैटरासाइक्लिन, इन दवाओं की चमत्कारी औषधियों को ‘‘वन्डर ड्रग्स’’ कहा जाता है। इनका मूल उद्देश्य है शरीर में उत्पन्न हुए या प्रवृष्ट हुए रोग कीटाणुओं को निरस्त करना। विकृत वैक्टीरियाओं—वायरसों के उपद्रव ही विभिन्न रोगों के प्रधान कारण माने जाते हैं। यह, मारक औषधियां इन कीटकों पर आक्रमण करती हैं—इन्हें मूर्छित करतीं और मारती हैं फलतः रोगों के जो कष्टकारक उपद्रव लक्षण थे वे शमन होते दिखाई देते हैं। इन मारक रसायनों के प्रयोग का उत्साह इसलिए ठंडा हो जाता है कि वे विषाणुओं के मारने के साथ रक्षाणुओं को भी नहीं बख्शती। उनकी दुधारी तलवार बिना अपने पराये का, मित्र-शत्रु का भेद-भाव किये जो भी उनकी पकड़ परिधि में आता है उन सभी का संहार करती है। पैनिसिलीन के चमत्कारी लाभों की आरम्भ में बहुत चर्चा थी, पर जब देखा गया कि उसके प्रयोग से दानेदार खुजली जैसे कितने ही नये रोग उत्पन्न होते हैं और किसी-किसी को तो उसकी प्रतिक्रिया प्राणघातक संकट ही उत्पन्न कर देती है। तब वह उत्साह ठंडा पड़ा। अब कुशल डॉक्टर पेनिसिलीन का प्रयोग आंखें मूंदकर नहीं करते। उसके लिए उन्हें फूंक फूंककर कदम धरना होता है। कुनैन से मलेरिया के जीवाणु तो मरते थे, पर कानों का बहरापन—नकसीर फूटना जैसे नये रोग गले बंध जाते हैं। इस असमंजस ने उसके प्रयोग का आरम्भिक उत्साह अब शिथिल कर दिया है। कुनैन का अन्धाधुन्ध प्रयोग अब नहीं किया जाता।
लन्दन के बारथोलोम्यूज अस्पताल में विभिन्न स्तर की एण्टी बायोटिक औषधियों का प्रयोग परीक्षण 275 प्रकार के बैक्टीरियाओं से ग्रसित मरीजों पर उलट-पुलट कर किया गया। इन परीक्षाओं में नव-निर्मित डी.एम.सी.टी. इस दृष्टि से अधिक प्रशंसनीय मानी गई कि उसने विषाणुओं का जितना संसार किया उतनी चोट रक्षाणुओं को नहीं पहुंचाई। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्णतया हानि रहित है। इसमें केवल रोग ही नष्ट होते हैं जीवनी शक्ति को क्षति नहीं पहुंचती ऐसा दावा करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं हो सका है।
हल्की खांसी, तीसरे पहर बुखार की हरारत, भूख की कमी, वजन का घटना, रात्रि के अन्तिम पहर में पसीना आना जैसे सामान्य लक्षणों से क्षय रोग की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है। इन चिन्हों के आधार पर यह आशंका की जा सकती है कि हो न हो रोगी पर क्षय का आक्रमण हो चला है।
वस्तुस्थिति का पता तो छाती का स्क्रीनिंग अथवा एक्सरे एवं रक्त, थूक आदि का परीक्षण करने पर ही चलता है। इसके लिए मांस मिनिएचर रेडियोग्राफी (एम.एम.आर.) की सरल परीक्षा पद्धति भी सामने आई है।
आमतौर से क्षय उपचार में लगातार दो-तीन महीने ‘स्टेप्टो माइसिन’ के इन्जेक्शन लगाये जाते हैं एव आइसोनेक्स—पी.ए.एस. जैसी दवाओं का स्थिति के अनुरूप सेवन कराया जाता है।
बचाव उपचार में बी.सी.जी. (वेसीलस काल्मेटेग्वेरिन) के टीके लगाये जाते हैं। यह नामकरण उनके आविष्कर्त्ताओं के नाम पर ही किया गया है। 40 सुइयों की खरोंच वाला यह टीका आरम्भ में बहुत उत्साहवर्धक समझा गया था, पर अब उसकी प्रतिक्रिया संदिग्ध आशंका के रूप में सामने आ रही है। अब क्षय से सुरक्षा प्राप्त करने का यह टीका अमोघ उपचार नहीं रहा वरन् उसके दुष्परिणाम पीछे किसी अन्य व्यथा को साथ लायेंगे ऐसे माना जाने लगा है।
आवश्यक नहीं कि आक्रमण बाहर से ही हों अपनी आन्तरिक दुर्बलता भी गृह युद्ध खड़ा कर देती है। ‘घर का भेदी लंका ढावे’ वाली कहावत भी बहुत बार सामने आती है। अवांछनीय व्यवहार से रुष्ट होकर अपने उपयोगी तत्व विद्रोही बनकर आक्रमणकारी शत्रु का रूप धारण कर लेते हैं और उस अन्तः विस्फोट का स्वरूप भी विप्लवी गृह युद्ध जैसे बन जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए रोगों और विषाणुओं की संख्या भी कम नहीं होती।
जब कारण वश शरीर के कुछेक जीवकोष विद्रोही हो जाते हैं तो सामान्य रीति-नीति की मान-मर्यादा तोड़कर उद्धत उच्छृंखल गतिविधि अपनाकर मनमर्जी की चाल चलते हैं। यह उद्धत विद्रोही ही केन्सर का मूल कारण हैं।
आमतौर से जीवकोष अपनी भूख तथा आवश्यकता तरल रक्त से प्राप्त करते रहते हैं किन्तु जब उनमें से कुछ असन्तुष्ट अपने लिए मनमर्जी का वैभव चाहते हैं तो समीपवर्ती जीवकोषों पर टूट पड़ते और उन्हें लूट-खसोटकर अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हैं इतना ही नहीं वे अपने लिए निर्धारित क्षेत्र और कार्य की मर्यादाओं को तोड़कर रक्त प्रवाह में तैरते हुए किसी भी अंग में जा घुसते हैं और वहां भी कत्लेआम का दृश्य उपस्थित करते हैं। जहां भी उन्हें पैर टिकाने को जगह मिली वहीं के अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं। यही है केन्सर की मूल प्रकृति।
केन्सर को उत्पन्न करने वाले उपकरण ‘कारसिनोज’ कहे जाते हैं। कोलतार, रेडियम, मादक द्रव्य इसी वर्ग में आते हैं। इनका गहरा प्रभाव शरीर पर पड़ेगा तो केन्सर की आशंका बढ़ेगी। अधिक आग तापने अथवा किसी अंग विशेष का अनावश्यक अतिघर्षण होते रहने से भी यह विपत्ति सामने आ खड़ी होती है। रतिक्रिया की सीमा एवं कोमलता का व्यतिक्रम होने से स्त्रियों की जननेन्द्रिय केन्सरग्रस्त हो जाती हैं।
एक ओर विषाणुओं की विभीषिका सामने खड़ी है और रुग्णता से लेकर मरण तक के साज संजो रही है वहां दूसरी ओर जीवन रक्षा की सेना भी कमर कसकर सामने खड़ी है। हमारे शरीर में ही एक विशालकाय महा भारत रचा हुआ है। कौरवों की कितनी ही अक्षौहिणी सेना जहां अपने दर्प से दहाड़ रही है वहां पाण्डवों की छोटी टुकड़ी भी आत्म-रक्षा के लिए प्राण हथेली पर रखकर युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। रक्ताणु हमारी जीवन रक्षा के अदम्य प्रहरी हैं वे विषाणुओं को परास्त करके जीवन सम्पदा को बचाने के लिए कट-कट कर लड़ते हैं अपने प्राण देकर के भी शत्रु का अपनी भूमि पर अधिकार न होने देने का प्रयत्न करते हैं हमारे अन्तः क्षेत्र में, धर्मक्षेत्र में, कर्मक्षेत्र में चलती रहने वाली यह महाभारत जैसी पुण्य प्रक्रिया देखने समझने ही योग्य है।
रक्त को नंगी आंखों से देखें तो वह लाल रंग का गाढ़ा प्रवाही मात्र दिखाई देता है, पर अणुवीक्षण यन्त्र से देखने पर उसमें असंख्य रक्ताणु दिखाई देते हैं। इनकी आकृति-प्रकृति की अब अनेकों जातियां जानी परखी जा चुकी हैं। यह रक्ताणु भी कोशिकाओं की तरह ही जन्मते-मरते रहते हैं। प्रायः उनकी आयु तीन महीने होती है। उनकी बनावट स्पंज सरीखी समझी जा सकती है जिसके रन्ध्रों में ‘हेमोग्लोविन’ नामक रसायन भरा होता है। यह रक्ताणु रक्त के साथ निरन्तर समस्त शरीर में भ्रमण करते रहते हैं और अपने तीन मास के स्वल्प जीवन काल में प्रायः तीन सौ मील का सफर कर लेते हैं।
हेमोग्लोविन कभी रक्त का प्रमुख रसायन माना जाता था। अब उसे चार श्रृंखलाओं में जुड़ा हुआ प्रायः 600 अमीनो अम्लों का समूह पाया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता लाइनस सी. पलिंग ने अपने दो साथियों के साथ इन रक्ताणुओं की शोध में अभिनव जानकारियों की कितनी ही कड़ियां जोड़ी हैं।
कितने ही रोग इन रक्ताणुओं के साथ जुड़े होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। कुछ विशेष कबीलों में कुछ विशेष प्रकार के रक्ताणु पाये जाते हैं तद्नुसार उनकी शारीरिक स्थिति में अमुक रोग का प्रतिरोध करने की—अमुक रोग से आक्रान्त होने की विशेष स्थिति देखी गई है। शारीरिक ही नहीं मानसिक क्षेत्र में भी यह रक्त विशेषता जमी रहती है। कुछ परिवारों के लोग बहुत भोले और डरपोक पाये जाते हैं जबकि किन्हीं वर्गों में आवेश, उत्तेजना और लड़ाकू प्रवृत्ति का बाहुल्य रहता है। राजपूतों की लड़ाकू प्रवृति और जुलाहों का डरपोकपन प्रसिद्ध है। सम्भवतः ऐसी विशेषताएं रक्ताणु की परम्परागत स्थिति के कारण उत्पन्न होती है।
पिछले पन्द्रह वर्षों में तीस से अधिक प्रकार के असामान्य हीमोग्लोबिन वर्गों का पता लगाया जा चुका है। केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो. वर्नाव एम. इंग्राम ने इनके वर्गीकरण तथा क्रियाकलापों की गहरी शोध करके यह पाया है कि शरीर एवं मन के रुग्ण एवं स्वस्थ होने में यह रक्त रसायन असाधारण भूमिका सम्पन्न करते हैं। अफ्रीका में कोई 80 हजार बच्चे इन रक्त रसायनों की विकृति के साथ जन्म लेने के कारण स्वल्प काल में ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इसी प्रकार उस महाद्वीप के एक कबीले में ऐसे रक्ताणु पाये गये जो मलेरिया के ‘प्लास्पोडियम फाल्सी पेरम’ कीटाणुओं से शरीर को तनिक भी प्रभावित नहीं होने देते। अन्य कबीलों के लोग उस क्षेत्र में आकर रहे तो तुरन्त मलेरिया ग्रसित हो गये किन्तु वहां के मूल निवासी मुद्दतों से इन्हीं मच्छरों के बीच रहते हुए कभी बीमार नहीं पड़े।
स्वीडन के शरीर विज्ञानी प्रो. फोलिंग इस बात पर जोर देते हैं कि विषाणुओं को मारने के लिए एन्टीवायटिक्स अथवा दूसरी प्रकार की जो मारक औषधियां दी जा रही हैं उनका प्रचलन बन्द किया जाय और स्वस्थ रक्ताओं को अधिक समर्थ बनाने के प्रयोगों को प्राथमिकता दी जाय। रोगों का स्थायी निवारण और सुदृढ़ स्वास्थ्य का संरक्षण इसी नीति को अपनाने से सम्भव होगा।
मारक औषधियां मित्र शत्रु का—अपने पराये का भेद किये बिना अपनी अन्धी तलवार दोनों पक्ष के योद्धाओं को मारने के लिए प्रयुक्त करती हैं। विषाणु मरें, सो ठीक है, पर स्वस्थ कणों की सम्पदा खोकर तो हम इतने दीन-हीन बन जाते हैं कि वह दुर्बलता भी रुग्णता से कम कष्टकारक नहीं होती। उससे भी मन्द गति से दीर्घकाल तक चलती रहने वाली रुग्णता ही जम बैठती है।
प्रकृति ने जीवन की प्रखरता को संजोये रखने के लिए संघर्ष आवश्यक समझा और विषाणुओं, रक्ताओं में निरन्तर संघर्ष होते रहने की व्यवस्था बनादी ताकि हम युद्ध कौशल में प्रवीण होकर सच्चे अर्थों में समर्थ और प्रगतिशील बन सकें।
इस युद्ध से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि शत्रु को मारने से भी अधिक उपयोगिता आत्म-पक्ष को सबल बनाने की है। संसार में फैली हुई अनीति के दमन के लिए आवेश में आकर उपयोगी-अनुपयोगी की परख किये बिना अन्धाधुन्ध तलवार चलना हानिकारक है। लाभ इसमें है कि नीति पक्ष को परिपुष्ट किया जाय जिससे बिना कठिन संघर्ष के ही शत्रु पक्ष परास्त हो सके साथ ही आत्म-पुष्टि से चिरस्थायी स्वास्थ्य सन्तुलन की—शान्ति और प्रगति की अभिवृद्धि हो सके। हमारी जीवन नीति एवं सुधार व्यवस्था का संचालन इसी आधार पर होना चाहिए।
असुरता के संहार में प्रवृत्त—अन्तः चेतना
कैंसर क्रोनिक स्टिमुलश से बढ़ता है, जिसका अधिकांश कारण धूम्रपान (स्मोकिंग) है। क्रोनिक सविसाइटिस (स्त्री-रोग), पेट का फोड़ा (पेष्टिक अल्सर) आदि से भी 5 प्रतिशत कैंसर हो सकता है। पर डाक्टरों की राय में इन सबका कारण अपनी ही चिन्तायें, उतावलापन और मिर्च-मसालों वाला गरिष्ठ आहार होता है। एक बार क्रोनिक स्टिमुलश पैदा हो जाने के बाद वह कोष (सेल्स) को विकृत करना प्रारम्भ करता है। 1 से 2, 2 से 4 इस क्षिप्र गति से बढ़ता हुआ यह रोग सारे शरीर पर उसी तरह छा जाता है जिस तरह दहेज रिश्वत, मिलावट, अन्धविश्वास, अशिक्षा और बाल-विवाह आदि कुरीतियां भारतीय जीवन को आच्छादित किये हैं। यदि प्रारम्भ में ही इसे नष्ट न किया गया तो कैंसर का ठीक होना कठिन हो जाता है।
मनुष्य जीवन की एक विस्तृत प्रक्रिया का नाम समाज है। हम जिस गांव में, मुहल्ले या नगर में रहते हैं—समाज वहीं तक सीमित नहीं। हमारा प्रान्त, हमारा देश, पड़ौसी देश और सारा विश्व एक समाज है। समाज की सीमायें विशाल हैं। अपने आप तक सीमित सुधार की प्रक्रियायें सरल हो सकती हैं किन्तु हम इस व्यापक समाज से इतने प्रभावित और बंधे हुए हैं कि उसकी हर छोटी-बड़ी बुराई से हमारा टकराव हर घड़ी होता रहता है। हमारी सज्जनता, हमारी शुद्धता, हमारा सौष्ठव तभी स्थिर रह सकता है जब सारा विश्व-समाज ही शुद्ध, सज्जन और सौम्य हो। इस जटिल समस्या को हल करना तभी सम्भव है जब विश्व-संस्कृति की सभी भलाई वाली शक्तियां निरन्तर क्रियाशील रहें और बुराइयों पर उसी प्रकार दबाव डालती रहें, जिस तरह शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग, शोक और बीमारियों का संहार औषधियों से करते रहते हैं। जब शरीर में बाहरी कीटाणुओं से या भीतरी किसी कारण से कोई रोग हो जाता है तो एन्टीबायटिक्स दवाइयों द्वारा उस पर सीधा घातक प्रभाव डाला जाता है। यह औषधियां शरीर के सारे रक्त का दौरा करती हैं और जहां कहीं भी रोग-कीटाणुओं को छिपा हुआ पाती हैं, मार गिराती हैं।
कई बार इस संघर्ष में अपनी भी हानि होती है। औषधि शास्त्र कहता है—यदि 100 शत्रु नष्ट करने में एक अपना भी मारा जाये तो कुछ हर्ज नहीं, पर सीधे मुकाबले का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। पेट में कई बार राउन्ड बाल्व्स पैदा हो जाते हैं। यह परजीवी (पैरासाइट) कीड़े (बैक्टीरिया) आंतों को उस तरह खाने लगते हैं जैसे फैशनपरस्ती, नशे-बाजी वासनायें स्वास्थ्य को खाने लगती हैं। इस स्थिति में डॉक्टर कोई दस्तावर औषधि देते हैं और रक्त में होने वाले विषैले प्रभाव से शरीर को बचाते हैं। इन औषधियों में तीव्रता होती है, वह पेट की सारी गन्दगी झाड़ फेंकती हैं। यह क्रिया कुछ तीव्र होती है, इससे पाचन वाले अम्ल (एसिड्स) भी पटक जाते हैं पर उनका चला जाना भी रोग के आक्रमण से हो जाने वाली हानि की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है। इसीलिये सीधे संघर्ष में कुछ लोगों को शारीरिक या मानसिक कष्ट भी हो, तो भी प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिए।
कई बार डॉक्टर उचित इलाज का पता नहीं लगा पाते, तब वे प्रभावित अंग से रोग के कीटाणु निकाल कर उन्हें कल्चर प्लेट पर रखते हैं और उन पर कई एन्टी बायोटिक्स औषधियों की एक-एक बूंद रखते जाते हैं। जो औषधि अधिक कीटाणुनाशक हुई, बाद में उसी का प्रयोग किया जाता है। बुराइयों से सतर्कता तो प्रत्येक स्थिति में रखनी ही चाहिए अन्यथा पता न चलेगा और वह भीतर ही भीतर हमें नष्ट कर दें सकती है। शराब पीने वालों में चर्बी की एक सतह जिगर के कोषों के ऊपर जम जाती है। उससे जिगर के कोषों को खाद्य (ऑक्सीजन) मिलना बन्द हो जाता है। शराब पीने वाले को पता नहीं चलता और भीतर-ही-भीतर सिरोसिस आफ लिवर बीमारी हो जाती है। मनुष्य को अपने स्वभाव, समाज की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। यदि ऐसा न हुआ और बीमारी पककर फूटी तो उसका संभालना कठिन हो जाता है।
डॉक्टर और स्वास्थ्य-विशेषज्ञ जानते हैं कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं—(1) एयरोबिक अर्थात् जिन्हें जिन्दा रहने के लिये ऑक्सीजन आवश्यक है। (2) एन एयरोबिक अर्थात् जिन्हें आवश्यक नहीं। कोई अंग सड़ जावे (ग्रैगीन) क्लास्टेडियम बेसलाई, क्लास्टेडियम एडेमेन्टीस एवम क्लास्टेडिक सेप्टिकी जो एन एयरोबिक हैं उनको मारने के लिये एयरोबिक वातावरण पैदा करना आवश्यक है।
बुराई न बढ़े, उसके लिये यह भी आवश्यक है कि उन्हें पोषण न मिले। गुण्डा तत्वों से डरकर लोग चाहते हुए भी उन्हीं का समर्थन और हां में हां मिलाने लगते हैं। इससे उनका कुनबा और भी फलने-फूलने लगता है। यदि लोग उनका समर्थन और पोषण बन्द कर दें तो वह अपने आप मरकर नष्ट हो जायें।
टी.बी. के कीटाणु इसी सिद्धांत पर मारे जाते हैं। यह एसिड फास्ट बेसिलाई [जो एसिड से भी नहीं मरते] हैं। जब इस तरह के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब डॉक्टर स्ट्रप्टोमाइसीन देते हैं। यह टी.बी. के कीटाणु की ऊपरी झिल्ली [लायपाइड कवरिंग] पर चारों ओर से घेरा डाल लेता है। इससे उस कीटाणु की मुसीबत आ जाती है। दुष्ट अपना खाद्य भी नहीं ले सकता और भीतर घुटकर मर जाता है। जो बुराइयां सीधी टक्कर से नहीं जीती जा सकतीं, उनको पोषण न मिले तो वे टी.बी. के कीटाणु की तरह आप नष्ट हो जाती हैं।
जहां इस स्थिति में भी काम न बने वहां भलाई की शक्ति का उद्बोधन करना और उसे मुकाबले के लिये ललकारना आवश्यक हो जाता है। नान स्पेसिफिक थैरेपी के अन्तर्गत कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो लगातार औषधि-सेवन से भी अच्छी नहीं होती। उदाहरण के लिये चमड़ी की बीमारी—एक्जिमा। उस स्थिति में डॉक्टर मुकाबले की शक्ति तैयार करते हैं। रोगी के शरीर का 5 सी.सी. शुद्ध रक्त लेकर रोगी के शरीर में प्रवेश [इन्जेक्ट] कर दिया जाता है। यह प्रोटीन होता है और भीतर शरीर में पहले से ही प्रोटीन होता है। जब तक अच्छाई बुराई में भेद न किया गया था, बुराई भी दहेज, पर्दा प्रथा, नशा आदि की तरह साथ-साथ पल रही थी। पर जब कुछ यज्ञ, हवन, जप, तप, बिना दहेज विवाह, नशा—उन्मूलन आदि की स्थिति बनी तो दूसरे लोगों ने भी अनुभव किया कि बुराई वह है जो अपनी या समाज के किसी भी वर्ग का अहित करती है भले ही वह कोई परम्परा बन गई हो। जब इस तरह का विवेक जाग पड़ता है तो अपनी बुराइयों का उन्मूलन ठीक ऐसे ही सरल हो जाता है, जैसे एक्जिमा में रोगी का ही रक्त इन्जेक्शन कर देना। भीतर वाले प्रोटोन उन्हें बाहरी समझ कर हमले के लिए तैयार होते हैं पर जब वे अनुभव करते हैं कि अरे! यह तो अपने ही बन्धु और हितैषी हैं तब उनसे मिल जाते हैं और एक नई शक्ति अनुभव करते हैं। अब सब मिलकर एक्जिमा के विरोध में लड़ पड़ते हैं और उस न मिटती जान पड़ने वाली बीमारी को भी नष्ट कर डालते हैं। अच्छाई को उकसाकर बुराई को नष्ट करने का प्रयोग बहुत ही उपयोगी और सफल सिद्ध होता रहा है।
यह वैज्ञानिक प्रयोग हैं जिनसे शरीर के समान ही अपने को शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। उसी के आधार पर सुख, समृद्धि और विश्वशान्ति का वातावरण पैदा किया जा सकता है।