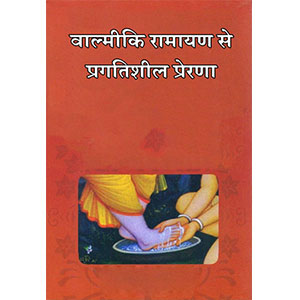वाल्मीकि रामायण से प्रगतिशील प्रेरणा 
आस्तिकता प्रकरण
आस्तिकता को ईश्वर विश्वास के नाम से भी कहा—समझा जाता है। ईश्वर का अर्थ कोई मूर्ति, व्यक्ति अथवा नाम विशेष न होकर एक उच्चतम, श्रेष्ठतम सर्वव्यापी सत्ता है, जिसे विभिन्न नामों और रूपों के माध्यम से याद रखने का प्रयास किया जाता है।
उच्चतम सत्ता के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण होना तथा उसको बराबर याद रखना मनुष्य के उत्थान और विकास के लिए आवश्यक है। अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ही मनुष्य उचित की उपेक्षा करके अनुचित रीति से सोचने और करने लग जाता है। यही उसकी व्यक्तिगत दुर्गति एवं सामाजिक पतन का कारण बनता है। ईश्वर के नाम से जानी समझी जाने वाली उच्चतम सत्ता उसके अनुरूप उदात्त भावनाओं, उत्कृष्ट विचारणाओं, श्रेष्ठ आदर्शों सिद्धान्त एवं नियम-मर्यादाओं के प्रति आस्थावान व्यक्ति स्वयं महान बनता है और अगणित मनुष्यों को सही राह पर बढ़ाने में सफल होता है।
ईश्वर के नाम से न सही श्रेष्ठ आदर्शों, मान्यताओं, नियमों एवं कर्तव्यों के रूप में भी उसका बोध और स्मरण किया जा सकता है। मनुष्य मात्र, प्राणि मात्र के प्रति सहानुभूति, सामाजिक आदर्शों, मानवीय सिद्धान्तों के रूप में भी उसे समझा और अपनाया जा सकता है। इसलिए उस सत्ता के प्रति तथा उससे सम्बन्धित व्यक्ति, भक्त, संत, महापुरुषों आदि के आचार विचारों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए तभी उसका लाभ ठीक प्रकार उठाया जा सकता है।
अवतारी पुरुष एवं उनके लक्षण—
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अवतार के उद्देश्य और सिद्धान्त को सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि परमात्मा तत्कालीन विकृतियों के समाधान के लिये किसी सर्वगुण सम्पन्न ऐसे व्यक्तित्व का सृजन कर देते हैं जो अपने पुरुषार्थ द्वारा समाज की विकृतियों का समाधान कर अपने नेतृत्व में लोगों को इच्छित दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तर काण्ड में वामन भगवान के संबंध में बलि कहते हैं—
प्रादुर्भावं विकुरुते येनैतन्निधन नयेत् । पुनरेवात्मनात्मानमधिष्ठाय स तिष्ठति ।।
ये किसी ऐसे को उत्पन्न कर देते हैं, जो उपद्रवी का नाश कर डालता है और यह स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही बने रहते हैं। अवतारी पुरुष अपनी श्रेष्ठता प्रकट करने के उद्देश्य से आचरण नहीं करते। उनका उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठता को जागृत करने का मर्म एवं ढंग उनको देखकर सीख सके। इसलिए वे अपने आपको सामान्य मनुष्य की मर्यादा में रखकर ही कार्य करते हैं। श्रीराम रावण-वध के बाद देवताओं से कहते हैं—
अब्रवीत्रिदशश्रेष्ठान्रामो धर्मभृतां वरः । आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ।।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम नाम का एक मनुष्य ही मानता हूं। किन्तु वे महान उद्देश्य को लेकर आते हैं और उसको पूरा करके ही जाते हैं। अपने लक्ष्य को वे भूलते नहीं। श्रीराम काल द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति की सूचना प्राप्त होने पर अपने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं—
त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम सम्भवतः । भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागतः ।।
तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने ही के लिये मेरा यह अवतार है। तुम्हारा मंगल हो। मैं जहां से आया हूं वहां ही चला जाऊंगा। जागृतात्मा व्यक्ति में भगवान की आभा प्रकट होती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और ईश्वर अपने आपको अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। अपनी वास्तविकता को न समझ पाने के कारण ही हम मूर्छित से रहते हैं। यदि हम अपनी शक्ति को समझ जायं तो कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। अवतारी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। लंका में युद्ध के समय लक्ष्मण चरित्र में यह तथ्य बड़ी सुन्दरता से उभरकर सामने आता है। लक्ष्मण जी युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गये। श्री राम ने उन्हें आत्म स्मरण कराया।
उन्हें बोध हुआ और—
आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः । विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् ।।
शत्रु हन्ता लक्ष्मण जी अपने को अचिन्त्य विष्णु भगवान का अंश समझ सचेत हुए। उनकी छाती का घाव पुर गया। अवतार के रूप में दिव्य सत्ता मानवी पुरुषार्थ के माध्यम से प्रस्फुरित होती है। अवतारी पुरुष इसीलिए मानवीय पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करते वरन् उसे बड़ी तत्परता से पूरा करते हैं। लक्ष्मण लंका युद्ध के अवसर पर श्रीराम को यही स्मरण दिलाते हुए कहते हैं—
दिव्यं च मानुषं च त्वमात्मनश्च पराक्रमम् । इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष्य यतस्व द्विषता वधे ।।
हे इक्ष्वाकुश्रेष्ठ! आप अपने दिव्य और मानवी पराक्रम की ओर देख कर, शत्रुवध का प्रयत्न कीजिये। भगवान् के अवतार का उद्देश्य धर्म रक्षा तथा अधर्म का नाश होता है, वे स्वतः तो अपने इस कर्तव्य को समझते ही हैं अन्य पात्र भी उसे जानते हैं। राक्षस मारीच रावण से कहता है—
रामो विग्रहवान्धर्मः साधु सत्यपराक्रमः । राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ।।
राम तो धर्म की साक्षात् मूर्ति हैं, वे बड़े साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जिस प्रकार इन्द्र देवताओं के नायक हैं, इसी प्रकार राम भी सब लोकों के नायक हैं। सत् पुरुष तो श्रीराम के इस रूप से परिचित हैं ही। रामायण के प्रारम्भ में ही महर्षि वाल्मीकि को राम का परिचय देते हुए नारद जी कहते हैं—
एष विग्रहवान्धर्म एष वीर्यवतां वरः । एष बुद्ध्याधिको लोके तपसश्च परायणम् ।।
वे धर्म की मूर्ति ही हैं, तथा तेजस्वी बुद्धिमान एवं लोक कल्याण के लिए सब प्रकार से तप साधना में तत्पर हैं। कर्तव्य परायणता ही धर्म है तथा संयम और सेवा द्वारा ही धर्म लाभ और उसका संरक्षण संभव है उसी प्रसंग में नारद कहते हैं—
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् ।।
वे धर्म के जानने वाले सत्य-प्रतिज्ञ प्रजा की भलाई करने वाले कीर्तिवान, ज्ञानी, पवित्र, मन और इन्द्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं।
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः । समुद्र इव गाम्भोर्ये धैर्येण हिमवानिव ।।
वे सद्गुणों के भण्डार, मां कौशल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले, समुद्र के समान गंभीर तथा हिमालय के समान धैर्यवान एवं दृढ़ हैं। राम में गुण एवं विभूतियां इतनी प्रखर दिखाई देती हैं कि उनकी उपमा मनुष्यों से नहीं दी जा सकती। उनमें अतिमानवीयता, ईश्वर की झलक मिलती है। नारद जी आगे कहते हैं—
विष्णुना सदृशो वोर्ये सामवत्प्रियदर्शनः । कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ।।
वे विष्णु के समन पराक्रमी, चन्द्रमा के समान शीतल एवं प्रिय, क्रोधित होने पर मृत्यु के समान, तथा पृथ्वी के समान क्षमा करने वाले हैं। धनुषयज्ञ के प्रकरण में राम की सफलता के बाद राजा जनक ऋषि विश्वामित्रजी से ऐसे ही भाव व्यक्त करते हैं—
भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । अत्यदभुत मचिन्त्यं च न तर्कितामिदं मया ।।
हे भगवन्! मैंने दशरथ पुत्र राम का अद्भुत, अचिन्त्य तथा तर्क से परे, पराक्रम देखा। महावीर हनुमान भी इन्हें इसी रूप में देखते हैं। अशोक वाटिका में वे सीताजी को आश्वासन देते हुए कहते हैं—
स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः । बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः ।।
जो उचित क्रोध कर दण्ड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ और महारथी हैं, जिनकी भुजा की छाया में रह कर लोग सुखी रहते हैं। उनके सहयोगी और भक्त ही नहीं उनके विरोधी राक्षस भी उनकी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। समुद्र के किनारे रामदल की सूचना देते हुए रावण के गुप्तचर रावण को बतलाते हैं—
यादृश तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च । वधिष्यति पुरीं लंकामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः ।।
जिस प्रकार का श्रीराम का रूप है जैसे उनके हथियार हैं; उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि श्रीराम अकेले ही लंका का नाश कर सकते हैं। लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी उनको आवश्यकता नहीं है।
रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् । दिव्यास्त्रगुणसम्पन्नः पुरन्दरसमा युधि ।।
हे रावण! श्रीरामचन्द्र बड़ा तेजस्वी और धनुषधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में दिव्यास्त्रों के चलाने में उसकी इन्द्र की तरह सामर्थ्य है।
यो भिन्द्याद्गगनं वाणैः पर्वतानपि दारयेत् । यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येय पराक्रमः ।।
जो अपने वाणों से आकाश को छेद सकते हैं और पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इन्द्र की तरह है।
यस्मिन्न चलते धर्मो यो धर्मान्नातिवर्तते । यो ब्राह्ममस्त्रं वेदश्च वेद वेदविदां वरः ।।
जो धर्म से न तो कभी डिगते हैं और न धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ही करते हैं, जो ब्रह्मास्त्र का चलाना जानते हैं, जो वेदों को केवल जानते ही नहीं, बल्कि वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं।
दूतों के वर्णन की सार्थकता लंका युद्ध में प्रत्यक्ष दिखलायी पड़ती है। राक्षस उनके युद्ध कौशल से चकित रह जाते हैं। उन्हें बार-बार लगता है कि एक नहीं हजारों राम युद्ध कर रहे हैं—
ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः । पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे ।।
कभी तो उन राक्षसों को युद्धभूमि को युद्धभूमि में हजारों श्रीरामचन्द्र दिखलाई पड़ते और कभी वे एक ही श्रीरामचन्द्र जी को देखते थे। असुरता के निवारण के लिए किये गये राम के संघर्ष की उपमा अन्यत्र नहीं मिलती यह तथ्य युद्ध देखने वाले गन्धर्व और अप्सराओं के मुख से व्यक्त होता है—
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव । एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्युद्धं रामरावणम् ।।
‘‘श्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीराम-रावण ही का युद्ध है’’ इस प्रकार कहते हुए वे सब श्रीरामचन्द्र और रावण का युद्ध देख रहे थे। अवतारी पुरुषों की आत्मीयता का विस्तार मनुष्य मात्र से आगे बढ़कर प्राणिमात्र तक हो जाता है। सीता खोज के प्रकरण में जामवंतजी वानरों को समझाते हुए कहते हैं—
तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगत्वतान्यपि । प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम् ।।
क्या पशु और क्या पक्षी, जितने प्राणी हैं, वे सब अपने प्राणों को देकर भी श्रीरामचन्द्रजी के प्रिय कार्य को वैसे ही करते हैं, जैसे कि हम सब। राम अपनी श्रेष्ठता का निर्वाह बराबर करते रहे, उन्हें कोई विचलित न कर सका। सीता वियोग की दुःख पूर्ण स्थिति आ पड़ने पर लक्ष्मणजी उनसे संतुलित रहने का आग्रह करते हुए उन्हें उन मूल विशेषताओं का स्मरण दिलाते हैं जिनसे व्यक्ति महान बनता है। लक्ष्मणजी कहते हैं कि हे राम आपको शोक में विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि—
भवा न्क्रयापरो लोके भावन्दैवपरायणः । आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायो व राघव ।।
आप कर्मठ है, दिव्यता को पोषण देने वाले हैं, आस्तिक हैं, धर्मशील हैं और उद्यमी हैं। श्री राम अपने गुणों के विकास और रक्षण के लिए सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। संध्योपासना-नियमादि का वे दृढ़ता से पालन करते हैं। विवाह के बाद श्री राम की दिनचर्या के सम्बन्ध में वाल्मीकि जी लिखते हैं—
तत्र श्रृण्वन्मुखा वाचः सूत मागध वन्दिनाम् । पूर्वां सन्ध्या मुपासीनो जजाप यतमानसः ।।
प्रातःकाल मागध, सूत और वन्दीजनों की मंगल वाणी सुनकर राम ने मन को नियन्त्रित कर प्रातः सन्ध्योपासन एवं गायत्री जप किया। राम का गायत्री जप और उपासना आदि केवल औपचारिक नहीं है। राम उन्हें जीवन में इस गहराई से अपनाते हैं कि वे तद्रूप हो जाते हैं। अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता उनसे प्राप्त कर दिखाते हैं। यहां तक कि वेद गायत्री आदि उनके अनुगामी बन जाते हैं। राम के महाप्रयाण प्रसंग में लिखा है—
वेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सर्वंरक्षिणी । ओंकारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुव्रताः ।।
ब्राह्मण रूप धारी वेद, सबकी रक्षा करने वाली गायत्री, ओंकार और वषट्कार सब राम के साथ-साथ चले। दिव्यता को इस स्तर तक जीवन में स्थान देने के कारण ही वे अपने महान उद्देश्य में सफल हो सके। नारदजी महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं—
बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्य सचराचरम् ।।
सब देवताओं से पूजित होकर राम संतुष्ट हुए। तथा उनके इस महान कार्य से तीनों लोकों के सभी प्राणियों का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्रीराम में मनुष्य शरीर की मर्यादाओं के ठीक-ठीक पालन के साथ-साथ ईश्वरीय शक्तियों का समावेश स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह कर संबोधित किया जाता है।
भक्ति और भगवान के सम्बन्ध—
भक्त रूप और वेष बनाने से ही नहीं बन जाते, वे पूरी तरह प्रभुसमर्पित जीवन जीते हैं। वे मानते हैं कि सारी शक्तियां और विभूतियां भगवान द्वारा उन्हीं का कार्य करने के लिए प्राप्त हुई हैं। अतः न तो वे उनका दुरुपयोग होने देते हैं, न सदुपयोग में ढिलाई होने देते हैं और न अपने कार्य के बदले में प्रभु से कुछ चाहते हैं। संसार की दृष्टि में वे अद्भुत पुरुषार्थ करते हैं, आत्म विश्वास पूर्वक बड़े से बड़ा कार्य कर दिखाते हैं, फिर भी कर्तापन का किंचित भी अहंकार नहीं होता, वे सारा श्रेय भगवान को ही देते हैं। भरत जी ऐसे ही भक्त हैं। राम वन-गमन के समय राज्य संचालन का उत्तरदायित्व वे स्वीकार तो कर लेते हैं किन्तु राजा स्वयं को नहीं प्रभु की पादुकाओं को ही मानते हैं। वे श्री राम से कहते हैं—
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ।।
हे आर्य! इन सुवर्ण भूषित पादुकाओं पर आप अपने चरण रखिये, क्योंकि ये ही दोनों खड़ाऊं सब के योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। भरत ने राज्य को राम की धरोहर समझा। पूरी, तत्परता से उसकी व्यवस्था की तथा वनवास के बाद राम के वापिस अयोध्या लौटने पर राज्य उन्हें सौंपते हुये कहा—
एतत्ते सकलं राज्य न्यासं निर्यातितं मया । अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृतश्च मनोरथः ।।
हे राजन्! इस राज्य को जो मेरे पास इतने दिनों से धरोहर रखा था, अब आप ग्रहण कर इसे सम्हालें। आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा मनोरथ भी पूरा हुआ। भरत यह संतोष किस आधार पर कर सके? वह है उनकी तत्परता जिससे उन्होंने भगवान द्वारा सौंपी संपत्ति एवं विभूतियों को अनेक गुणा बढ़ा लिया, निस्पृह भाव से उस पर अपना अधिकार न मानते हुए उन्हें ही सौंप दिया। भरत के शब्द हैं—
भवतस्तेजसा सर्व कृतं दशगुणं मया । तथा ब्रुवाणं भरतं दृष्ट्वा तं भ्रतृवत्सलम् ।।
आपके प्रताप से मैंने पहले से सब दस गुने अधिक बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार कहते हुये भ्रातृवत्सल भरत को देख (राक्षसराज विभीषण तथा वानरों की आंखों से आंसू निकल आये।)
अपने को भगवान का भक्त कहने वाला हर व्यक्ति यदि इसी प्रकार उनके द्वारा प्रदत्त विभूतियों को बढ़ाकर उन्हीं के अर्पित कर सके तो उनकी भक्ति सार्थक हो जाय, जीवन धन्य हो जाय।
हर भक्त के लिए कुछ विशेष भूमिका निर्धारित रहती है, उसे निभाने के लिए उसे बहुत सतर्क रहना होता है। भक्त हनुमान सीता की खोज में अकेले ही लंका में घुस जाते हैं किन्तु भावावेश में बहक नहीं जाते। वे अपने कर्तव्य की गम्भीरता को समझते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। उन्हें शरीर का मोह नहीं किन्तु यह चिन्ता है कि भगवान का कार्य अधूरा न रह जाय, वे सोचते हैं—
नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । विमृशंश्च न पश्यामि यो हत मयि व नरः ।।
बहुत सोचने पर भी मैं ऐसा कोई दूसरा नहीं देख पाता जो मेरे मारे जाने पर श्रीराम के कार्य को पूरा करने में उनका उपयुक्त सहायक सिद्ध हो सके। यही सोचकर वे अपने प्राणों की रक्षा की सावधानी बरतते हैं। वैसे उन्हें मान अपमान, शारीरिक कष्ट आदि का कोई भय नहीं। राक्षसों की पकड़ में वे आ जाते हैं राक्षस उन्हें अपमानित करते और सताते हैं तो वे सोचने लगते हैं—
किंतु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम् । लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति ।।
श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं इस प्रकार के अनादर को भी सह लूंगा। ये लोग मुझे लंका में धुमावें तो इससे अच्छा ही होगा। ऐसे भक्तों को कोई भी कष्ट नहीं होता। अपनी पूंछ में लगी हुई आग द्वारा पूरी लंका जला देने पर भी हनुमान की पूंछ में आग का असर नहीं हुआ। वे यह तथ्य समझते हैं—
नूनं रामप्रभावेन वैदेह्याः सुकृतेन च । यन्मां दहनकमांऽयं नादहद्धव्यवाहनः ।।
तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप और सीता जी के पुण्य-प्रभाव से जलाने वाले अग्नि ने मुझे नहीं जलाया—यह निश्चय बात है। ऐसे भक्तों को ही भगवान अपना विश्वासपात्र बनाते हैं और उनका सहारा लेकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। लंका विजय के लिये वानरी सेना के प्रस्थान करते समय राम युद्ध की योजना बनाते हुए सुग्रीव से कहते हैं—
यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिहर्षयन् । अधिरुह्य हनूमन्तमैरावतमिवेश्वरः ।।
मैं हनुमान के कंधे पर सवार हो, ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इन्द्र की तरह, सेना के मध्यभाग में रह कर सेना को हर्षित अथवा उत्साहित करता हुआ चलूंगा। हनुमान की तरह निस्पृह, समर्पित भावना से कार्य करने वाले भक्तों के प्रति भगवान बड़ा आदर का भाव रखते हैं, उनका बहुत अनुग्रह मानते है। लंका में अकेले सफलता से अपना कार्य करके लौटे हुए हनुमान के प्रति उनके भाव हैं—
इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कुर्मि सदृश प्रियम् ।।
इस घड़ी मुझ दीन को एक बात बहुत सता रही है। वह यह है कि मैं इस प्रिय संवाद देने वाले हनुमान को इस कार्य के अनुरूप कुछ भी पारितोषिक नहीं दे सकता। भगवान भक्त के समर्पण के बदले में स्वयं को भक्त के प्रति समर्पित कर देते हैं। भक्त हनुमान के कार्य का यही पारितोषिक वे उचित समझते हुए कहते है—
एष सवंस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ।
जो हो, इस समय, मेरा यह सर्वस्वदान रूप आलिंगन ही महात्मा (महाबली) हनुमान जी के कार्य के योग्य पुरस्कार है।
इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे । हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतम् ।।
महात्मा (महाबली) और काम पूरा कर के आये हुए हनुमान जी से यह कहकर और प्रीति-पुलकित शरीर से, श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमान को अपने गले लगा लिया। यह बात श्रीराम भूल नहीं जाते अयोध्या लौटने पर राज्याभिषेक के बाद वे हनुमान से कहते हैं—
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ।।
हे वानर! तुम्हारे एक ही उपकार पर (प्रसन्न हो) मैं तुम्हें अपने प्राणदान करता हूं। तुम्हारे बचे हुए उपकारों के लिये हम लोग तुम्हारे ऋणी बने रहेंगे। भगवान की कृतज्ञता भी कितनी उच्चकोटि की है? अपना सब कुछ भक्त को देकर भी अपने को ऋणी मानते हैं। यही नहीं वे चाहते हैं कि यह ऋण कभी उतरे भी नहीं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त कभी किसी से, स्वयं उनसे भी कुछ लेने की स्थिति में न रहे, देने की स्थिति में ही बना रहे। वे कहते हैं—
मदङ्गेजीर्णतां यातु यत्वयोपकृतं कपे । नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम् ।।
हे वानर! तुमने जो उपकार किये हैं, वे मेरे अंगों में जीर्ण हो जायं, क्योंकि मनुष्य आपत्तियों ही में प्रत्युपकार के पात्र हुआ करते हैं। अथवा जो तुमने मेरे प्रति उपकार किये हैं वे सब मेरे हृदय में बने रहेंगे। क्योंकि उपकारी के प्रति बिना, उस पर विपत्ति पड़े, प्रत्युपकार किया नहीं जा सकता (और मैं यह नहीं चाहता कि तुम पर कभी विपत्ति पड़े।) भगवान् के साथ-साथ ऐसे भक्तों की कीर्ति भी अमिट हो जाती है। अपने महाप्रयाण से पूर्व राम ने हनुमान से कहा—
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर । तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन् ।।
हे वानरराज! जब तक इस लोक में मेरी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम हर्षित हो मर्त्यलोक में वास करना। भगवान और भक्तों के इन संबंधों पर विचार कर हमें भी वास्तविक भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए।
उच्चतम सत्ता के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण होना तथा उसको बराबर याद रखना मनुष्य के उत्थान और विकास के लिए आवश्यक है। अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ही मनुष्य उचित की उपेक्षा करके अनुचित रीति से सोचने और करने लग जाता है। यही उसकी व्यक्तिगत दुर्गति एवं सामाजिक पतन का कारण बनता है। ईश्वर के नाम से जानी समझी जाने वाली उच्चतम सत्ता उसके अनुरूप उदात्त भावनाओं, उत्कृष्ट विचारणाओं, श्रेष्ठ आदर्शों सिद्धान्त एवं नियम-मर्यादाओं के प्रति आस्थावान व्यक्ति स्वयं महान बनता है और अगणित मनुष्यों को सही राह पर बढ़ाने में सफल होता है।
ईश्वर के नाम से न सही श्रेष्ठ आदर्शों, मान्यताओं, नियमों एवं कर्तव्यों के रूप में भी उसका बोध और स्मरण किया जा सकता है। मनुष्य मात्र, प्राणि मात्र के प्रति सहानुभूति, सामाजिक आदर्शों, मानवीय सिद्धान्तों के रूप में भी उसे समझा और अपनाया जा सकता है। इसलिए उस सत्ता के प्रति तथा उससे सम्बन्धित व्यक्ति, भक्त, संत, महापुरुषों आदि के आचार विचारों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए तभी उसका लाभ ठीक प्रकार उठाया जा सकता है।
अवतारी पुरुष एवं उनके लक्षण—
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अवतार के उद्देश्य और सिद्धान्त को सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि परमात्मा तत्कालीन विकृतियों के समाधान के लिये किसी सर्वगुण सम्पन्न ऐसे व्यक्तित्व का सृजन कर देते हैं जो अपने पुरुषार्थ द्वारा समाज की विकृतियों का समाधान कर अपने नेतृत्व में लोगों को इच्छित दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तर काण्ड में वामन भगवान के संबंध में बलि कहते हैं—
प्रादुर्भावं विकुरुते येनैतन्निधन नयेत् । पुनरेवात्मनात्मानमधिष्ठाय स तिष्ठति ।।
ये किसी ऐसे को उत्पन्न कर देते हैं, जो उपद्रवी का नाश कर डालता है और यह स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही बने रहते हैं। अवतारी पुरुष अपनी श्रेष्ठता प्रकट करने के उद्देश्य से आचरण नहीं करते। उनका उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठता को जागृत करने का मर्म एवं ढंग उनको देखकर सीख सके। इसलिए वे अपने आपको सामान्य मनुष्य की मर्यादा में रखकर ही कार्य करते हैं। श्रीराम रावण-वध के बाद देवताओं से कहते हैं—
अब्रवीत्रिदशश्रेष्ठान्रामो धर्मभृतां वरः । आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ।।
धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम नाम का एक मनुष्य ही मानता हूं। किन्तु वे महान उद्देश्य को लेकर आते हैं और उसको पूरा करके ही जाते हैं। अपने लक्ष्य को वे भूलते नहीं। श्रीराम काल द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति की सूचना प्राप्त होने पर अपने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं—
त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम सम्भवतः । भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामि यत एवाहमागतः ।।
तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने ही के लिये मेरा यह अवतार है। तुम्हारा मंगल हो। मैं जहां से आया हूं वहां ही चला जाऊंगा। जागृतात्मा व्यक्ति में भगवान की आभा प्रकट होती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और ईश्वर अपने आपको अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। अपनी वास्तविकता को न समझ पाने के कारण ही हम मूर्छित से रहते हैं। यदि हम अपनी शक्ति को समझ जायं तो कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। अवतारी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। लंका में युद्ध के समय लक्ष्मण चरित्र में यह तथ्य बड़ी सुन्दरता से उभरकर सामने आता है। लक्ष्मण जी युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गये। श्री राम ने उन्हें आत्म स्मरण कराया।
उन्हें बोध हुआ और—
आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः । विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् ।।
शत्रु हन्ता लक्ष्मण जी अपने को अचिन्त्य विष्णु भगवान का अंश समझ सचेत हुए। उनकी छाती का घाव पुर गया। अवतार के रूप में दिव्य सत्ता मानवी पुरुषार्थ के माध्यम से प्रस्फुरित होती है। अवतारी पुरुष इसीलिए मानवीय पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करते वरन् उसे बड़ी तत्परता से पूरा करते हैं। लक्ष्मण लंका युद्ध के अवसर पर श्रीराम को यही स्मरण दिलाते हुए कहते हैं—
दिव्यं च मानुषं च त्वमात्मनश्च पराक्रमम् । इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष्य यतस्व द्विषता वधे ।।
हे इक्ष्वाकुश्रेष्ठ! आप अपने दिव्य और मानवी पराक्रम की ओर देख कर, शत्रुवध का प्रयत्न कीजिये। भगवान् के अवतार का उद्देश्य धर्म रक्षा तथा अधर्म का नाश होता है, वे स्वतः तो अपने इस कर्तव्य को समझते ही हैं अन्य पात्र भी उसे जानते हैं। राक्षस मारीच रावण से कहता है—
रामो विग्रहवान्धर्मः साधु सत्यपराक्रमः । राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ।।
राम तो धर्म की साक्षात् मूर्ति हैं, वे बड़े साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जिस प्रकार इन्द्र देवताओं के नायक हैं, इसी प्रकार राम भी सब लोकों के नायक हैं। सत् पुरुष तो श्रीराम के इस रूप से परिचित हैं ही। रामायण के प्रारम्भ में ही महर्षि वाल्मीकि को राम का परिचय देते हुए नारद जी कहते हैं—
एष विग्रहवान्धर्म एष वीर्यवतां वरः । एष बुद्ध्याधिको लोके तपसश्च परायणम् ।।
वे धर्म की मूर्ति ही हैं, तथा तेजस्वी बुद्धिमान एवं लोक कल्याण के लिए सब प्रकार से तप साधना में तत्पर हैं। कर्तव्य परायणता ही धर्म है तथा संयम और सेवा द्वारा ही धर्म लाभ और उसका संरक्षण संभव है उसी प्रसंग में नारद कहते हैं—
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् ।।
वे धर्म के जानने वाले सत्य-प्रतिज्ञ प्रजा की भलाई करने वाले कीर्तिवान, ज्ञानी, पवित्र, मन और इन्द्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं।
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः । समुद्र इव गाम्भोर्ये धैर्येण हिमवानिव ।।
वे सद्गुणों के भण्डार, मां कौशल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले, समुद्र के समान गंभीर तथा हिमालय के समान धैर्यवान एवं दृढ़ हैं। राम में गुण एवं विभूतियां इतनी प्रखर दिखाई देती हैं कि उनकी उपमा मनुष्यों से नहीं दी जा सकती। उनमें अतिमानवीयता, ईश्वर की झलक मिलती है। नारद जी आगे कहते हैं—
विष्णुना सदृशो वोर्ये सामवत्प्रियदर्शनः । कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ।।
वे विष्णु के समन पराक्रमी, चन्द्रमा के समान शीतल एवं प्रिय, क्रोधित होने पर मृत्यु के समान, तथा पृथ्वी के समान क्षमा करने वाले हैं। धनुषयज्ञ के प्रकरण में राम की सफलता के बाद राजा जनक ऋषि विश्वामित्रजी से ऐसे ही भाव व्यक्त करते हैं—
भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । अत्यदभुत मचिन्त्यं च न तर्कितामिदं मया ।।
हे भगवन्! मैंने दशरथ पुत्र राम का अद्भुत, अचिन्त्य तथा तर्क से परे, पराक्रम देखा। महावीर हनुमान भी इन्हें इसी रूप में देखते हैं। अशोक वाटिका में वे सीताजी को आश्वासन देते हुए कहते हैं—
स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः । बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोको महात्मनः ।।
जो उचित क्रोध कर दण्ड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ और महारथी हैं, जिनकी भुजा की छाया में रह कर लोग सुखी रहते हैं। उनके सहयोगी और भक्त ही नहीं उनके विरोधी राक्षस भी उनकी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। समुद्र के किनारे रामदल की सूचना देते हुए रावण के गुप्तचर रावण को बतलाते हैं—
यादृश तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च । वधिष्यति पुरीं लंकामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः ।।
जिस प्रकार का श्रीराम का रूप है जैसे उनके हथियार हैं; उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि श्रीराम अकेले ही लंका का नाश कर सकते हैं। लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी उनको आवश्यकता नहीं है।
रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् । दिव्यास्त्रगुणसम्पन्नः पुरन्दरसमा युधि ।।
हे रावण! श्रीरामचन्द्र बड़ा तेजस्वी और धनुषधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में दिव्यास्त्रों के चलाने में उसकी इन्द्र की तरह सामर्थ्य है।
यो भिन्द्याद्गगनं वाणैः पर्वतानपि दारयेत् । यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येय पराक्रमः ।।
जो अपने वाणों से आकाश को छेद सकते हैं और पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इन्द्र की तरह है।
यस्मिन्न चलते धर्मो यो धर्मान्नातिवर्तते । यो ब्राह्ममस्त्रं वेदश्च वेद वेदविदां वरः ।।
जो धर्म से न तो कभी डिगते हैं और न धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ही करते हैं, जो ब्रह्मास्त्र का चलाना जानते हैं, जो वेदों को केवल जानते ही नहीं, बल्कि वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं।
दूतों के वर्णन की सार्थकता लंका युद्ध में प्रत्यक्ष दिखलायी पड़ती है। राक्षस उनके युद्ध कौशल से चकित रह जाते हैं। उन्हें बार-बार लगता है कि एक नहीं हजारों राम युद्ध कर रहे हैं—
ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसाः । पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे ।।
कभी तो उन राक्षसों को युद्धभूमि को युद्धभूमि में हजारों श्रीरामचन्द्र दिखलाई पड़ते और कभी वे एक ही श्रीरामचन्द्र जी को देखते थे। असुरता के निवारण के लिए किये गये राम के संघर्ष की उपमा अन्यत्र नहीं मिलती यह तथ्य युद्ध देखने वाले गन्धर्व और अप्सराओं के मुख से व्यक्त होता है—
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव । एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्युद्धं रामरावणम् ।।
‘‘श्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीराम-रावण ही का युद्ध है’’ इस प्रकार कहते हुए वे सब श्रीरामचन्द्र और रावण का युद्ध देख रहे थे। अवतारी पुरुषों की आत्मीयता का विस्तार मनुष्य मात्र से आगे बढ़कर प्राणिमात्र तक हो जाता है। सीता खोज के प्रकरण में जामवंतजी वानरों को समझाते हुए कहते हैं—
तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगत्वतान्यपि । प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम् ।।
क्या पशु और क्या पक्षी, जितने प्राणी हैं, वे सब अपने प्राणों को देकर भी श्रीरामचन्द्रजी के प्रिय कार्य को वैसे ही करते हैं, जैसे कि हम सब। राम अपनी श्रेष्ठता का निर्वाह बराबर करते रहे, उन्हें कोई विचलित न कर सका। सीता वियोग की दुःख पूर्ण स्थिति आ पड़ने पर लक्ष्मणजी उनसे संतुलित रहने का आग्रह करते हुए उन्हें उन मूल विशेषताओं का स्मरण दिलाते हैं जिनसे व्यक्ति महान बनता है। लक्ष्मणजी कहते हैं कि हे राम आपको शोक में विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि—
भवा न्क्रयापरो लोके भावन्दैवपरायणः । आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायो व राघव ।।
आप कर्मठ है, दिव्यता को पोषण देने वाले हैं, आस्तिक हैं, धर्मशील हैं और उद्यमी हैं। श्री राम अपने गुणों के विकास और रक्षण के लिए सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। संध्योपासना-नियमादि का वे दृढ़ता से पालन करते हैं। विवाह के बाद श्री राम की दिनचर्या के सम्बन्ध में वाल्मीकि जी लिखते हैं—
तत्र श्रृण्वन्मुखा वाचः सूत मागध वन्दिनाम् । पूर्वां सन्ध्या मुपासीनो जजाप यतमानसः ।।
प्रातःकाल मागध, सूत और वन्दीजनों की मंगल वाणी सुनकर राम ने मन को नियन्त्रित कर प्रातः सन्ध्योपासन एवं गायत्री जप किया। राम का गायत्री जप और उपासना आदि केवल औपचारिक नहीं है। राम उन्हें जीवन में इस गहराई से अपनाते हैं कि वे तद्रूप हो जाते हैं। अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता उनसे प्राप्त कर दिखाते हैं। यहां तक कि वेद गायत्री आदि उनके अनुगामी बन जाते हैं। राम के महाप्रयाण प्रसंग में लिखा है—
वेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सर्वंरक्षिणी । ओंकारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुव्रताः ।।
ब्राह्मण रूप धारी वेद, सबकी रक्षा करने वाली गायत्री, ओंकार और वषट्कार सब राम के साथ-साथ चले। दिव्यता को इस स्तर तक जीवन में स्थान देने के कारण ही वे अपने महान उद्देश्य में सफल हो सके। नारदजी महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं—
बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्य सचराचरम् ।।
सब देवताओं से पूजित होकर राम संतुष्ट हुए। तथा उनके इस महान कार्य से तीनों लोकों के सभी प्राणियों का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्रीराम में मनुष्य शरीर की मर्यादाओं के ठीक-ठीक पालन के साथ-साथ ईश्वरीय शक्तियों का समावेश स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह कर संबोधित किया जाता है।
भक्ति और भगवान के सम्बन्ध—
भक्त रूप और वेष बनाने से ही नहीं बन जाते, वे पूरी तरह प्रभुसमर्पित जीवन जीते हैं। वे मानते हैं कि सारी शक्तियां और विभूतियां भगवान द्वारा उन्हीं का कार्य करने के लिए प्राप्त हुई हैं। अतः न तो वे उनका दुरुपयोग होने देते हैं, न सदुपयोग में ढिलाई होने देते हैं और न अपने कार्य के बदले में प्रभु से कुछ चाहते हैं। संसार की दृष्टि में वे अद्भुत पुरुषार्थ करते हैं, आत्म विश्वास पूर्वक बड़े से बड़ा कार्य कर दिखाते हैं, फिर भी कर्तापन का किंचित भी अहंकार नहीं होता, वे सारा श्रेय भगवान को ही देते हैं। भरत जी ऐसे ही भक्त हैं। राम वन-गमन के समय राज्य संचालन का उत्तरदायित्व वे स्वीकार तो कर लेते हैं किन्तु राजा स्वयं को नहीं प्रभु की पादुकाओं को ही मानते हैं। वे श्री राम से कहते हैं—
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ।।
हे आर्य! इन सुवर्ण भूषित पादुकाओं पर आप अपने चरण रखिये, क्योंकि ये ही दोनों खड़ाऊं सब के योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। भरत ने राज्य को राम की धरोहर समझा। पूरी, तत्परता से उसकी व्यवस्था की तथा वनवास के बाद राम के वापिस अयोध्या लौटने पर राज्य उन्हें सौंपते हुये कहा—
एतत्ते सकलं राज्य न्यासं निर्यातितं मया । अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृतश्च मनोरथः ।।
हे राजन्! इस राज्य को जो मेरे पास इतने दिनों से धरोहर रखा था, अब आप ग्रहण कर इसे सम्हालें। आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा मनोरथ भी पूरा हुआ। भरत यह संतोष किस आधार पर कर सके? वह है उनकी तत्परता जिससे उन्होंने भगवान द्वारा सौंपी संपत्ति एवं विभूतियों को अनेक गुणा बढ़ा लिया, निस्पृह भाव से उस पर अपना अधिकार न मानते हुए उन्हें ही सौंप दिया। भरत के शब्द हैं—
भवतस्तेजसा सर्व कृतं दशगुणं मया । तथा ब्रुवाणं भरतं दृष्ट्वा तं भ्रतृवत्सलम् ।।
आपके प्रताप से मैंने पहले से सब दस गुने अधिक बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार कहते हुये भ्रातृवत्सल भरत को देख (राक्षसराज विभीषण तथा वानरों की आंखों से आंसू निकल आये।)
अपने को भगवान का भक्त कहने वाला हर व्यक्ति यदि इसी प्रकार उनके द्वारा प्रदत्त विभूतियों को बढ़ाकर उन्हीं के अर्पित कर सके तो उनकी भक्ति सार्थक हो जाय, जीवन धन्य हो जाय।
हर भक्त के लिए कुछ विशेष भूमिका निर्धारित रहती है, उसे निभाने के लिए उसे बहुत सतर्क रहना होता है। भक्त हनुमान सीता की खोज में अकेले ही लंका में घुस जाते हैं किन्तु भावावेश में बहक नहीं जाते। वे अपने कर्तव्य की गम्भीरता को समझते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। उन्हें शरीर का मोह नहीं किन्तु यह चिन्ता है कि भगवान का कार्य अधूरा न रह जाय, वे सोचते हैं—
नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । विमृशंश्च न पश्यामि यो हत मयि व नरः ।।
बहुत सोचने पर भी मैं ऐसा कोई दूसरा नहीं देख पाता जो मेरे मारे जाने पर श्रीराम के कार्य को पूरा करने में उनका उपयुक्त सहायक सिद्ध हो सके। यही सोचकर वे अपने प्राणों की रक्षा की सावधानी बरतते हैं। वैसे उन्हें मान अपमान, शारीरिक कष्ट आदि का कोई भय नहीं। राक्षसों की पकड़ में वे आ जाते हैं राक्षस उन्हें अपमानित करते और सताते हैं तो वे सोचने लगते हैं—
किंतु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम् । लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति ।।
श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं इस प्रकार के अनादर को भी सह लूंगा। ये लोग मुझे लंका में धुमावें तो इससे अच्छा ही होगा। ऐसे भक्तों को कोई भी कष्ट नहीं होता। अपनी पूंछ में लगी हुई आग द्वारा पूरी लंका जला देने पर भी हनुमान की पूंछ में आग का असर नहीं हुआ। वे यह तथ्य समझते हैं—
नूनं रामप्रभावेन वैदेह्याः सुकृतेन च । यन्मां दहनकमांऽयं नादहद्धव्यवाहनः ।।
तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप और सीता जी के पुण्य-प्रभाव से जलाने वाले अग्नि ने मुझे नहीं जलाया—यह निश्चय बात है। ऐसे भक्तों को ही भगवान अपना विश्वासपात्र बनाते हैं और उनका सहारा लेकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। लंका विजय के लिये वानरी सेना के प्रस्थान करते समय राम युद्ध की योजना बनाते हुए सुग्रीव से कहते हैं—
यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिहर्षयन् । अधिरुह्य हनूमन्तमैरावतमिवेश्वरः ।।
मैं हनुमान के कंधे पर सवार हो, ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इन्द्र की तरह, सेना के मध्यभाग में रह कर सेना को हर्षित अथवा उत्साहित करता हुआ चलूंगा। हनुमान की तरह निस्पृह, समर्पित भावना से कार्य करने वाले भक्तों के प्रति भगवान बड़ा आदर का भाव रखते हैं, उनका बहुत अनुग्रह मानते है। लंका में अकेले सफलता से अपना कार्य करके लौटे हुए हनुमान के प्रति उनके भाव हैं—
इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कुर्मि सदृश प्रियम् ।।
इस घड़ी मुझ दीन को एक बात बहुत सता रही है। वह यह है कि मैं इस प्रिय संवाद देने वाले हनुमान को इस कार्य के अनुरूप कुछ भी पारितोषिक नहीं दे सकता। भगवान भक्त के समर्पण के बदले में स्वयं को भक्त के प्रति समर्पित कर देते हैं। भक्त हनुमान के कार्य का यही पारितोषिक वे उचित समझते हुए कहते है—
एष सवंस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः । मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ।
जो हो, इस समय, मेरा यह सर्वस्वदान रूप आलिंगन ही महात्मा (महाबली) हनुमान जी के कार्य के योग्य पुरस्कार है।
इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे । हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतम् ।।
महात्मा (महाबली) और काम पूरा कर के आये हुए हनुमान जी से यह कहकर और प्रीति-पुलकित शरीर से, श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमान को अपने गले लगा लिया। यह बात श्रीराम भूल नहीं जाते अयोध्या लौटने पर राज्याभिषेक के बाद वे हनुमान से कहते हैं—
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ।।
हे वानर! तुम्हारे एक ही उपकार पर (प्रसन्न हो) मैं तुम्हें अपने प्राणदान करता हूं। तुम्हारे बचे हुए उपकारों के लिये हम लोग तुम्हारे ऋणी बने रहेंगे। भगवान की कृतज्ञता भी कितनी उच्चकोटि की है? अपना सब कुछ भक्त को देकर भी अपने को ऋणी मानते हैं। यही नहीं वे चाहते हैं कि यह ऋण कभी उतरे भी नहीं। वे चाहते हैं कि उनका भक्त कभी किसी से, स्वयं उनसे भी कुछ लेने की स्थिति में न रहे, देने की स्थिति में ही बना रहे। वे कहते हैं—
मदङ्गेजीर्णतां यातु यत्वयोपकृतं कपे । नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम् ।।
हे वानर! तुमने जो उपकार किये हैं, वे मेरे अंगों में जीर्ण हो जायं, क्योंकि मनुष्य आपत्तियों ही में प्रत्युपकार के पात्र हुआ करते हैं। अथवा जो तुमने मेरे प्रति उपकार किये हैं वे सब मेरे हृदय में बने रहेंगे। क्योंकि उपकारी के प्रति बिना, उस पर विपत्ति पड़े, प्रत्युपकार किया नहीं जा सकता (और मैं यह नहीं चाहता कि तुम पर कभी विपत्ति पड़े।) भगवान् के साथ-साथ ऐसे भक्तों की कीर्ति भी अमिट हो जाती है। अपने महाप्रयाण से पूर्व राम ने हनुमान से कहा—
मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर । तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन् ।।
हे वानरराज! जब तक इस लोक में मेरी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम हर्षित हो मर्त्यलोक में वास करना। भगवान और भक्तों के इन संबंधों पर विचार कर हमें भी वास्तविक भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए।