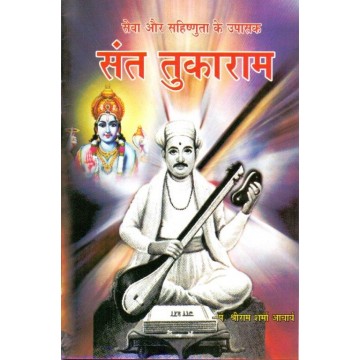संत तुकाराम 
मन को जीतना सबसे बडा़ पुरूषार्थ
Read Scan Version
तुकाराम ने अपने मन को वश में करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया था और
उन्होंने अन्य अध्यात्म-प्रेमियों को यही उपदेश दिया है मनोजय के बिना
आत्मजय की बात करना दंभ मात्र है। पर मन को जीतना सहज नहीं और यही कारण है
कि सार्वभौम सम्राटों की अपेक्षा भी अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाले एक
लंगोटीधारी साधु को संसार में अधिक महत्व दिया जाता है। इस तथ्य को समझाते
हुए तुकाराम ने कहा-
मन करा रे प्रसन्न, सर्व सिद्धि चे साधन।
मोक्ष अथवा बंधन, सुख समाधान इच्छातें।।
अर्थात्- "भाईयों ! मन को प्रसन्न करो, जो कि सब सिद्धियों का मूल और बंधन तथा मोक्ष का कारण है। उसको स्वायत करके ही सुख की इच्छा की जा सकती है।"
आगे चलकर वे कहते हैं "मन पर अंकुश रखना चाहिए कि जिससे जाग्रति का नित्य नवीन दिवस उदय होता रहे।" पर यह बात कहने में जितनी सहज है, उतनी ही करने में कठिन है, इस बात को भी तुकारम बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने भगवान् से बार-बार यही प्रार्थना की है कि वे उन्हें मन को वश में करने कि शक्ति दें। इस दृष्टि से वे निरंकुश मन की निंदा करते हुए कहते हैं- "मन को रोकने की इच्छा करें तो भी यह स्वेच्छाचारी नहीं रुकता। मेरा मन मुझे ही हानि पहुँचाता है। इसके भीतर सांसारिक प्रपंच भरा है, भक्ति तो बाहर ही दिखलाई पड़ती है। इसलिए हे भगवान् ! इस मन को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। इस मन के कारण हे भगवान् मैं बहुत ही दुःखी हूँ। क्या मन के इन विकारों को आप भी नहीं रोक सकते? इसने मेरे मार्ग में काम, क्रोध के पर्वत खडे़ कर दिये हैं, जिससे भगवान् दूसरी तरफ ही रह गये। मैं इन पहाडो़ को लाँघ नहीं सकता और कोई रास्ता भी दिखलाई नहीं पड़ता। अब नारायण मेरे सुहृद कहाँ रहे? वे तो मुझे छोड़कर चल दिये। मन ऐसा चंचल है कि एक घडी़ या एक पल भी स्थिर नहीं रहता। इसको मैंने बहुत रोका, बाँधकर रखा, पर इससे ये और भी बिगड़ने लगता है और चाहे जहाँ भागता है। इसको न भजन प्रिय लगता है और न शास्त्र-कथा रुचिकर जान पड़ती है। यह तो केवल विषयों की तरफ ही दौड़ता है।"
धन, कामवासना और मान-
अध्यात्म-मार्ग में धन, कामवासना और मान तीन बड़ी खाइयाँ हैं। प्रथम तो इस मार्ग पर चलने वाले यात्री ही थोड़े होते हैं। फिर जो होते भी हैं, वे पहली खाई अर्थात- अर्थ लिप्सा में ही गायब हो जाते हैं। जो बचे रहते हैं। वे दूसरी खाई- कामवासना में डूब जाते हैं। इससे भी बचकर जो आगे बढ़ते हैं, वे तीसरी खाई- यश की लालसा में खप जाते हैं। जो इन तीनों खाइयों को पार कर जाते हैं, वे ही अध्यात्म के शिखर पर पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं।
तुकाराम का मनःसंयम बड़ा प्रचंड था, इससे पहली दो खाइयों को तो वह सहज ही पार कर गये। पर तीसरी के पार करने में उन्हें भी कुछ कठिनाई हुई, ऐसा जान पड़ता है। सबसे पहले धन की खाई आती है, परंतु तुकाराम ने वैराग्य की प्रथम अवस्था में ही 'धन को पत्थर के समान ही नहीं वरन् गोमांस के समान' मानने का निश्चय कर लिया था। शिवाजी महाराज ने उनके उपदेशों से तृप्त होकर हीरा, मोती सुवर्ण मुद्राएँ भेंट स्वरूप भेजी थीं, पर तुकाराम ने उनको देखा भी नहीं, ज्यों का त्यों वापस कर दिया। वैराग्य होने के पश्चात् वे धन के संबंध में निर्लिप्त रहे।
दूसरा मोह कामवासना का होता है। यद्यपि तुकाराम अंत तक गृहस्थ बने रहे, पर उन्होंने किसी स्त्री को वासना के भाव से कभी नहीं देखा। उनकी दिनचर्या भी ऐसी थी कि रात्रि के समय 'विठ्ठल-मंदिर में कीर्तन समाप्त होते- होते बारह बज जाते थे। और फिर वे कठिनता से तीन-चार घंटे सो सकते थे। वह भी कभी मंदिर में ही सोते रहते, कभी घर आ जाते। फिर ऊषाकाल में ही उठकर स्नान करके श्री विठ्ठल की पूजा करते और सूर्योदय होते ही किसी पर्वत के ऊपर जा बैठते और वहाँ से प्रायः संध्या तक वापस आते। इस दिनचर्या मे स्त्री से मिलने का अवसर कदाचित् ही मिलता था। जिस पुरूष में ऐसी प्रखर वैराग्य भावना हो, वह अन्य स्त्रियों की कामना कैसे कर सकता है? पर पुरूष से प्रेम करने वाली स्त्रियाँ तो रीछनी के समान लगती थीं-
तुका म्हणे तैसा दिसतील नारी।
रिसाचिय परि आम्ह पुढे़।।
अर्थात- "ऐसी चरित्रहीन स्त्रियाँ मेरे सम्मुख आयें तो मुझे वे रीछनी जैसी जान पड़ती हैं। "जिस प्रकार रीछनी खून चूसकर प्राण हर लेती हैं, उसी प्रकार इस तरह की स्त्रियों का संपर्क परमार्थी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि "अध्यात्मवादी मनुष्य को प्राण जाने पर भी स्त्रियों के साथ वासनायुक्त वार्तालाप नहीं करना चाहिए। "जिस साधक में इतनी दृढ़ता होगी, उसी का वैराग्य टिक सकता है। इसकी कमी के फलस्वरूप ही अनेक 'गुरू बाबाजी' और 'महात्मा' दया, परोपकार, नारी-उद्धार की बातें करते-करते कहीं से कहीं जा पहुँचते हैं। तुकाराम और समर्थ गुरू रामदास जैसे सच्चे संयमी सत्पुरूषों का ही काम है कि वे स्त्री-जाती की उन्नति के उपाय करें, अधकचरे व्यक्तियों के बस की यह बात नहीं है। जिन्होंने अपना ही उद्धार नहीं किया, वे दूसरों का उद्धार क्या करेंगे? वे तो उन्नति और उद्धार के नाम पर अपनी और दूसरों की अधोगति ही करेंगें।
जिस समय तुकाराम भंडारा पर्वत पर ईश्वर-ध्यान में निमग्न रहते थे, उस समय एक रूपवती स्त्री अपने मन से या किसी अन्य के कहने से उनकी परीक्षा करने एकांत में पहुँची। उस समय तुकाराम ने एक अभंग में उस स्त्री को अपने मन के भाव इस प्रकार बतलाये- "पर मेरे लिए रुक्मिणी माता के समान है, यह मेरा सदा से निश्चय है। इसलिए हे माता ! तुम जाओ और मेरे लिए कुछ प्रयत्न करो। हम तो विष्णु के दास हैं। तुम्हारा यह पतन मुझसे सहन नहीं होता। तुम फिर कभी ऐसी खराब बात मुख से मत निकालना। "इस प्रकार तुकाराम ने उसे रुक्मिणी- माता बनाकर विदा कर दिया।
मनुष्य मात्र मान की इच्छा करते हैं। अन्य व्यक्ति हमको अच्छा कहें और हमारी बातों को सम्मानपूर्वक सुनें, यह कौन नहीं चाहता? केवल दो तरह के व्यक्ति ही ऐसे होते हैं, जिन्हें मान की परवाह नहीं होती। एक तो दुर्व्यसनों और दुराचार में हद दर्जे तक फँसे हुए और दूसरे वे जो आत्म शुद्धि की दृष्टि से निंदा और स्तुति को समान समझ लेते हैं। तुकाराम ने जन-समाज की सम्मति की परवाह न करके सत्यासत्य का निर्णय अपनी आत्मा द्वारा ही किया और उसी पर आगे बढ़ते चले गये, जन-समाज को त्यागने का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अन्य लोगों के प्रति दया, करुणा, परोपकार के भाव को छोड़ दिया हो, पर दुनियादार लोग जो विवेकशून्य बातें किया करते हैं और कोई मनुष्य परमार्थ के भाव से भी कार्य करे, उसमें भी दोष ढूँढ़ने की ही चेष्टा करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना उन्होंने व्यर्थ समझ लिया। उन्होंने इस विषय में कहा-
"मैं केवल अपना ही विचार करूँ तो ठीक है, क्योंकि अन्य लोगों के उद्धार की चर्चा करने पर भी, वे तो उदासीन ही रहते हैं। अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे हरिकीर्तन के लिए कहा जाये तो उनको बुरा लगता है। हरिकीर्तन को कोई सुने या न सुने, चाहे तो वह घर जाकर सुख से सो जाय, पर मैं तो अपने लिए प्रभु से करुणा की प्रार्थना करूँगा ही। जिसकी जैसी भावना होगी, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा।"
शुभ कर्म में बाधा डालने वाले-इस प्रकार जब तुकाराम आत्म शुद्धि और आंतरिक शांति के लिए हरिकीर्तन करने लगे और जनता को भगवत्- भक्ति का उपदेश देना आरंभ किया तो अनेक लोग उनके पास आकर तरह-तरह के तर्क-कुतर्क करने लगे वे तरह- तरह के सिद्धान्त उपस्थित करके उनसे वाद-विवाद करने लगते। तरह-तरह कि शंकाएँ उठाते इस पर उन्होंने कहा-
" मैं किस आधार पर विचार करूँ? मेरे चित्त को कौन धीरज बँधायेगा? संतो के आदेशानुसार मैं भगवान् के गुण गाता हूँ- सेवा-धर्म पर चलता हूँ। मैं शास्त्रवेत्ता नहीं हूँ, वेदवेत्ता नहीं हूँ, सामान्य क्षुद्र जीव हूँ। पर लोग आकर मुझे तंग करते हैं, मुझ में बुद्धिभेद उत्पन्न करना चाहते हैं और कहते हैं- 'भगवान् तो निराकार हैं- निर्गुण हैं। इसलिये हे भगवान् ! अब तुम्हीं बताओ कि मैं तुम्हारा भजन करूँ या न करूँ ?"
मैं किसी के घर भीख माँगने नहीं जाता, फिर भी कंटक मुझे दुःख देने को जबर्दस्ती आ जाते हैं। मैं न तो किसी का कुछ खाता हूँ और न किसी का कुछ बिगाड़ता हूँ, फिर भी पाखंडी लोग मेरे पीछे पडे़ हैं। जिस बात को मैं नहीं जानता उसे वे मुझे छलपूर्वक पूछते हैं। मैं उनके चरणों में पड़ता हूँ तो भी वे नहीं छोड़ते। अपने अकेले जीव से मैं किस-किस से विवाद करूं? तेरे गुण बखानूँ- यथाशक्ति सेवा करूँ या कुतर्कीजनों के साथ बहस करूँ? एक मुख से मैं क्या-क्या करूँ?"
तुकाराम सीधे, सरल स्वभाव के भक्त थे। उनके सेवा-भाव और हृदय से निकले हरिकीर्तन के प्रभाव से जनता के बहुसंख्यक व्यक्ति उनके पास सुनने को आते और उनका सम्मान करते। इससे पुराने ढंग के पंडितों को ईर्ष्या होती थी। वे अपने को शास्त्रों का ठेकेदार और बहुत उच्च समझते थे, पर इस अंह-वृत्ति के कारण साधारण जनता के व्यक्ति उनके पास बहुत कम जाते थे। तुकाराम उनको अपने में से ही एक जान पड़ते थे, उनकी बातें भी खूब समझ सकते थे। इसलिए उनके कीर्तन में झुंड के झुंड लोग आ जाते थे। इससे पंडितों के मन में जलन होती थी और वे तरह-तरह के प्रश्न करके तुकाराम से बहस करना चाहते थे, जिससे उन्हें नीचा देखना पडे़। पर तुकाराम ने तो भक्ति और सेवा का सरल मार्ग अपनाया था, उन्हें शास्त्रों के शुष्क वितंडावाद से क्या मतलब? इसलिए अकारण समय नष्ट करने के व्यवहार से वे दुःखी होते थे और उससे बचाने की भगवान् से प्रार्थना करते थे।
तुकाराम ने सैकड़ों अभंगों में अपने को हर प्रकार से नीच, कपटी, पापी, दोषी प्रकट किया है और भगवान् से शरण देने की प्रार्थना की है। अनेक लोग इन बातों को निर्रथक मानते हैं, पर संत इनके द्वारा अपनी अहंवृत्ति पर विजय पाने कि चेष्टा करते हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है और अनेक बार सज्जन और भले व्यक्तियों के भी पतन का कारण बन जाता है। दूसरा कारण यह भी था कि वे स्वयं ही अपने को दीन-हीन और दूषित मानते थे, जिससे दूसरों के दोष ढूँढ़ने वाले आलोचकों और बडे़ बनने वाले अहंकारियों की निगाह से बचे रहें।
मन करा रे प्रसन्न, सर्व सिद्धि चे साधन।
मोक्ष अथवा बंधन, सुख समाधान इच्छातें।।
अर्थात्- "भाईयों ! मन को प्रसन्न करो, जो कि सब सिद्धियों का मूल और बंधन तथा मोक्ष का कारण है। उसको स्वायत करके ही सुख की इच्छा की जा सकती है।"
आगे चलकर वे कहते हैं "मन पर अंकुश रखना चाहिए कि जिससे जाग्रति का नित्य नवीन दिवस उदय होता रहे।" पर यह बात कहने में जितनी सहज है, उतनी ही करने में कठिन है, इस बात को भी तुकारम बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने भगवान् से बार-बार यही प्रार्थना की है कि वे उन्हें मन को वश में करने कि शक्ति दें। इस दृष्टि से वे निरंकुश मन की निंदा करते हुए कहते हैं- "मन को रोकने की इच्छा करें तो भी यह स्वेच्छाचारी नहीं रुकता। मेरा मन मुझे ही हानि पहुँचाता है। इसके भीतर सांसारिक प्रपंच भरा है, भक्ति तो बाहर ही दिखलाई पड़ती है। इसलिए हे भगवान् ! इस मन को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। इस मन के कारण हे भगवान् मैं बहुत ही दुःखी हूँ। क्या मन के इन विकारों को आप भी नहीं रोक सकते? इसने मेरे मार्ग में काम, क्रोध के पर्वत खडे़ कर दिये हैं, जिससे भगवान् दूसरी तरफ ही रह गये। मैं इन पहाडो़ को लाँघ नहीं सकता और कोई रास्ता भी दिखलाई नहीं पड़ता। अब नारायण मेरे सुहृद कहाँ रहे? वे तो मुझे छोड़कर चल दिये। मन ऐसा चंचल है कि एक घडी़ या एक पल भी स्थिर नहीं रहता। इसको मैंने बहुत रोका, बाँधकर रखा, पर इससे ये और भी बिगड़ने लगता है और चाहे जहाँ भागता है। इसको न भजन प्रिय लगता है और न शास्त्र-कथा रुचिकर जान पड़ती है। यह तो केवल विषयों की तरफ ही दौड़ता है।"
धन, कामवासना और मान-
अध्यात्म-मार्ग में धन, कामवासना और मान तीन बड़ी खाइयाँ हैं। प्रथम तो इस मार्ग पर चलने वाले यात्री ही थोड़े होते हैं। फिर जो होते भी हैं, वे पहली खाई अर्थात- अर्थ लिप्सा में ही गायब हो जाते हैं। जो बचे रहते हैं। वे दूसरी खाई- कामवासना में डूब जाते हैं। इससे भी बचकर जो आगे बढ़ते हैं, वे तीसरी खाई- यश की लालसा में खप जाते हैं। जो इन तीनों खाइयों को पार कर जाते हैं, वे ही अध्यात्म के शिखर पर पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं।
तुकाराम का मनःसंयम बड़ा प्रचंड था, इससे पहली दो खाइयों को तो वह सहज ही पार कर गये। पर तीसरी के पार करने में उन्हें भी कुछ कठिनाई हुई, ऐसा जान पड़ता है। सबसे पहले धन की खाई आती है, परंतु तुकाराम ने वैराग्य की प्रथम अवस्था में ही 'धन को पत्थर के समान ही नहीं वरन् गोमांस के समान' मानने का निश्चय कर लिया था। शिवाजी महाराज ने उनके उपदेशों से तृप्त होकर हीरा, मोती सुवर्ण मुद्राएँ भेंट स्वरूप भेजी थीं, पर तुकाराम ने उनको देखा भी नहीं, ज्यों का त्यों वापस कर दिया। वैराग्य होने के पश्चात् वे धन के संबंध में निर्लिप्त रहे।
दूसरा मोह कामवासना का होता है। यद्यपि तुकाराम अंत तक गृहस्थ बने रहे, पर उन्होंने किसी स्त्री को वासना के भाव से कभी नहीं देखा। उनकी दिनचर्या भी ऐसी थी कि रात्रि के समय 'विठ्ठल-मंदिर में कीर्तन समाप्त होते- होते बारह बज जाते थे। और फिर वे कठिनता से तीन-चार घंटे सो सकते थे। वह भी कभी मंदिर में ही सोते रहते, कभी घर आ जाते। फिर ऊषाकाल में ही उठकर स्नान करके श्री विठ्ठल की पूजा करते और सूर्योदय होते ही किसी पर्वत के ऊपर जा बैठते और वहाँ से प्रायः संध्या तक वापस आते। इस दिनचर्या मे स्त्री से मिलने का अवसर कदाचित् ही मिलता था। जिस पुरूष में ऐसी प्रखर वैराग्य भावना हो, वह अन्य स्त्रियों की कामना कैसे कर सकता है? पर पुरूष से प्रेम करने वाली स्त्रियाँ तो रीछनी के समान लगती थीं-
तुका म्हणे तैसा दिसतील नारी।
रिसाचिय परि आम्ह पुढे़।।
अर्थात- "ऐसी चरित्रहीन स्त्रियाँ मेरे सम्मुख आयें तो मुझे वे रीछनी जैसी जान पड़ती हैं। "जिस प्रकार रीछनी खून चूसकर प्राण हर लेती हैं, उसी प्रकार इस तरह की स्त्रियों का संपर्क परमार्थी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि "अध्यात्मवादी मनुष्य को प्राण जाने पर भी स्त्रियों के साथ वासनायुक्त वार्तालाप नहीं करना चाहिए। "जिस साधक में इतनी दृढ़ता होगी, उसी का वैराग्य टिक सकता है। इसकी कमी के फलस्वरूप ही अनेक 'गुरू बाबाजी' और 'महात्मा' दया, परोपकार, नारी-उद्धार की बातें करते-करते कहीं से कहीं जा पहुँचते हैं। तुकाराम और समर्थ गुरू रामदास जैसे सच्चे संयमी सत्पुरूषों का ही काम है कि वे स्त्री-जाती की उन्नति के उपाय करें, अधकचरे व्यक्तियों के बस की यह बात नहीं है। जिन्होंने अपना ही उद्धार नहीं किया, वे दूसरों का उद्धार क्या करेंगे? वे तो उन्नति और उद्धार के नाम पर अपनी और दूसरों की अधोगति ही करेंगें।
जिस समय तुकाराम भंडारा पर्वत पर ईश्वर-ध्यान में निमग्न रहते थे, उस समय एक रूपवती स्त्री अपने मन से या किसी अन्य के कहने से उनकी परीक्षा करने एकांत में पहुँची। उस समय तुकाराम ने एक अभंग में उस स्त्री को अपने मन के भाव इस प्रकार बतलाये- "पर मेरे लिए रुक्मिणी माता के समान है, यह मेरा सदा से निश्चय है। इसलिए हे माता ! तुम जाओ और मेरे लिए कुछ प्रयत्न करो। हम तो विष्णु के दास हैं। तुम्हारा यह पतन मुझसे सहन नहीं होता। तुम फिर कभी ऐसी खराब बात मुख से मत निकालना। "इस प्रकार तुकाराम ने उसे रुक्मिणी- माता बनाकर विदा कर दिया।
मनुष्य मात्र मान की इच्छा करते हैं। अन्य व्यक्ति हमको अच्छा कहें और हमारी बातों को सम्मानपूर्वक सुनें, यह कौन नहीं चाहता? केवल दो तरह के व्यक्ति ही ऐसे होते हैं, जिन्हें मान की परवाह नहीं होती। एक तो दुर्व्यसनों और दुराचार में हद दर्जे तक फँसे हुए और दूसरे वे जो आत्म शुद्धि की दृष्टि से निंदा और स्तुति को समान समझ लेते हैं। तुकाराम ने जन-समाज की सम्मति की परवाह न करके सत्यासत्य का निर्णय अपनी आत्मा द्वारा ही किया और उसी पर आगे बढ़ते चले गये, जन-समाज को त्यागने का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अन्य लोगों के प्रति दया, करुणा, परोपकार के भाव को छोड़ दिया हो, पर दुनियादार लोग जो विवेकशून्य बातें किया करते हैं और कोई मनुष्य परमार्थ के भाव से भी कार्य करे, उसमें भी दोष ढूँढ़ने की ही चेष्टा करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना उन्होंने व्यर्थ समझ लिया। उन्होंने इस विषय में कहा-
"मैं केवल अपना ही विचार करूँ तो ठीक है, क्योंकि अन्य लोगों के उद्धार की चर्चा करने पर भी, वे तो उदासीन ही रहते हैं। अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे हरिकीर्तन के लिए कहा जाये तो उनको बुरा लगता है। हरिकीर्तन को कोई सुने या न सुने, चाहे तो वह घर जाकर सुख से सो जाय, पर मैं तो अपने लिए प्रभु से करुणा की प्रार्थना करूँगा ही। जिसकी जैसी भावना होगी, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा।"
शुभ कर्म में बाधा डालने वाले-इस प्रकार जब तुकाराम आत्म शुद्धि और आंतरिक शांति के लिए हरिकीर्तन करने लगे और जनता को भगवत्- भक्ति का उपदेश देना आरंभ किया तो अनेक लोग उनके पास आकर तरह-तरह के तर्क-कुतर्क करने लगे वे तरह- तरह के सिद्धान्त उपस्थित करके उनसे वाद-विवाद करने लगते। तरह-तरह कि शंकाएँ उठाते इस पर उन्होंने कहा-
" मैं किस आधार पर विचार करूँ? मेरे चित्त को कौन धीरज बँधायेगा? संतो के आदेशानुसार मैं भगवान् के गुण गाता हूँ- सेवा-धर्म पर चलता हूँ। मैं शास्त्रवेत्ता नहीं हूँ, वेदवेत्ता नहीं हूँ, सामान्य क्षुद्र जीव हूँ। पर लोग आकर मुझे तंग करते हैं, मुझ में बुद्धिभेद उत्पन्न करना चाहते हैं और कहते हैं- 'भगवान् तो निराकार हैं- निर्गुण हैं। इसलिये हे भगवान् ! अब तुम्हीं बताओ कि मैं तुम्हारा भजन करूँ या न करूँ ?"
मैं किसी के घर भीख माँगने नहीं जाता, फिर भी कंटक मुझे दुःख देने को जबर्दस्ती आ जाते हैं। मैं न तो किसी का कुछ खाता हूँ और न किसी का कुछ बिगाड़ता हूँ, फिर भी पाखंडी लोग मेरे पीछे पडे़ हैं। जिस बात को मैं नहीं जानता उसे वे मुझे छलपूर्वक पूछते हैं। मैं उनके चरणों में पड़ता हूँ तो भी वे नहीं छोड़ते। अपने अकेले जीव से मैं किस-किस से विवाद करूं? तेरे गुण बखानूँ- यथाशक्ति सेवा करूँ या कुतर्कीजनों के साथ बहस करूँ? एक मुख से मैं क्या-क्या करूँ?"
तुकाराम सीधे, सरल स्वभाव के भक्त थे। उनके सेवा-भाव और हृदय से निकले हरिकीर्तन के प्रभाव से जनता के बहुसंख्यक व्यक्ति उनके पास सुनने को आते और उनका सम्मान करते। इससे पुराने ढंग के पंडितों को ईर्ष्या होती थी। वे अपने को शास्त्रों का ठेकेदार और बहुत उच्च समझते थे, पर इस अंह-वृत्ति के कारण साधारण जनता के व्यक्ति उनके पास बहुत कम जाते थे। तुकाराम उनको अपने में से ही एक जान पड़ते थे, उनकी बातें भी खूब समझ सकते थे। इसलिए उनके कीर्तन में झुंड के झुंड लोग आ जाते थे। इससे पंडितों के मन में जलन होती थी और वे तरह-तरह के प्रश्न करके तुकाराम से बहस करना चाहते थे, जिससे उन्हें नीचा देखना पडे़। पर तुकाराम ने तो भक्ति और सेवा का सरल मार्ग अपनाया था, उन्हें शास्त्रों के शुष्क वितंडावाद से क्या मतलब? इसलिए अकारण समय नष्ट करने के व्यवहार से वे दुःखी होते थे और उससे बचाने की भगवान् से प्रार्थना करते थे।
तुकाराम ने सैकड़ों अभंगों में अपने को हर प्रकार से नीच, कपटी, पापी, दोषी प्रकट किया है और भगवान् से शरण देने की प्रार्थना की है। अनेक लोग इन बातों को निर्रथक मानते हैं, पर संत इनके द्वारा अपनी अहंवृत्ति पर विजय पाने कि चेष्टा करते हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है और अनेक बार सज्जन और भले व्यक्तियों के भी पतन का कारण बन जाता है। दूसरा कारण यह भी था कि वे स्वयं ही अपने को दीन-हीन और दूषित मानते थे, जिससे दूसरों के दोष ढूँढ़ने वाले आलोचकों और बडे़ बनने वाले अहंकारियों की निगाह से बचे रहें।