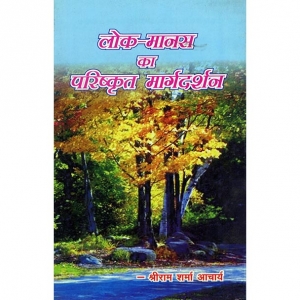लोक-मानस का परिष्कृत मार्गदर्शन 
देकर पाने वाले सच्चे भगवद् भक्त लोक-सेवी
Read Scan Version
भगवान की भक्ति के नाम पर लोग ऐसी विडम्बनायें रचते रहते हैं, जिसमें पूजा-पाठ जैसी कुछ खिलवाड़ तो होती रहे, पर बदले में ऋद्धि-सिद्धियां, चमत्कारों और वरदानों का जखीरा लूट के माल की तरह हाथ लगे। कई स्वर्ग और मुक्ति का वैभव स्वर्ग लोक में पहुंचकर बटोरना चाहते हैं। कइयों को दर्शन की इच्छा होती है मानो किसी रूपसी की समीपता का रसास्वादन करना चाहते हों। दस पैसे की मिठाई मनौती के लिए चढ़ाकर मालामाल बनने और मुफ्त में बढ़-चढ़कर सफलतायें प्राप्त करने की हविश तो इस समुदाय के अधिकांश लोगों को होती है। कहीं-कहीं रात भर नाचकूद चलते हैं ताकि भगवान की नींद हराम करके जितना कुछ लपक सकना संभव हो, लपक लिया जाय। बच्चों को बहलाने-फुसलाने या चिड़ियां-मछलियां पकड़ने की धूर्तता तो कितने ही करते हैं। भगवान की दुकान को आंखों में धूल झोंककर लूट लाने का कुचक्र तो उस क्षेत्र में आमतौर से रचे जाते देखा जा सकता है।
यथार्थता की कसौटी पर कसे जाने के उपरान्त स्पष्ट होता है कि भगवान का दरबार ‘‘अन्धेर नगरी-बेबूझ राजा’’ की उक्ति चरितार्थ नहीं करता। वहां उन्हीं को अनुकम्पा का अनुदान मिलता है, जिन्हें प्रामाणिकता और उदारता की कसौटी पर खरा कस लिया जाता है। भक्ति का सीधा अर्थ होता है—सेवा अर्थात् लोक मंगल। यह उन्हीं से बन पड़ता है, जो अपने को हर दृष्टि से संयम की आग में तपाते हैं। औसत नागरिक का जीवन जीकर उससे ऐसा कुछ बचा लेते हैं जिसे समयदान, अंशदान के रूप में दरिद्र नारायण के चरणों पर अर्पित किया जा सके। सत्प्रवृत्ति संवर्धन में उसका बढ़ा-चढ़ा उपयोग किया जा सके। सच्चे भगवद्-भक्त इसी स्तर के होते रहे हैं और बदले में आत्म संतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह का प्रत्यक्ष प्रतिफल उपलब्ध करते रहे हैं।
सुदामा का उदाहरण सामने है। उनका विशालकाय गुरुकुल था। सुयोग्य अध्यापन और वातावरण जहां भी होगा, वहां छात्रों की कमी न रहेगी। पुरातन काल में गुरुकुल-विश्वविद्यालय ही छात्रों के शिक्षण और निर्वाह की दुहरी व्यवस्था वहन करते थे, पर उस क्षेत्र में उदारचेताओं की कमी पड़ जाने से गुरुकुलों के ऊपर भारी आर्थिक कठिनाई लदी रहने लगी। आसरा किसका लिया जाय। सोचा गया कि भगवान को पकड़ा जाय। वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने स्थिति को जाना और अपनी सम्पदा कुटुम्बियों के विलास हेतु छोड़ने की अपेक्षा यह उचित समझा कि जो पास में है वह सब कुछ उच्च आदर्श के हेतु विसर्जित कर दिया जाय। द्वारिकापुरी की सारी सम्पदा उठकर सुदामापुरी चली आयी। लक्ष्मीनारायण की अनुकम्पा ऐसों को ही प्राप्त होती है। जेबकटी का रास्ता अपनाने वालों को नहीं।
भक्तों में एक आते हैं—विभीषण। उनने अनीति में सगे भाई का भी साथ नहीं दिया। अपमान और अभाव सहते रहे और समय आने पर अपनी समूची वफादारी उस न्याय और नीति के पक्ष में समर्पित कर दी, जिसे प्रकारान्तर से भगवान कहते हैं। भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। उसे सोने की लंका और अद्वितीय विदुषी मन्दोदरी का लाभ मिला। ऐसे ही प्रसंग सिद्ध करते हैं कि भगवान भक्त-वत्सल और विभूतियों के अधिपति हैं।
सच्चे भक्तों की श्रेणी में सुग्रीव का नाम आता है। राम के साथ अनीति हुई। दुष्टों ने सीताहरण कर लिया। खोजने के लिए दूतों और लड़ने के लिए सैनिकों की आवश्यकता हुई। भक्त सुग्रीव ने जो कुछ भी अपने पास था मुक्त हस्त से दिया। दानी की खाली हुई जेबें भगवान भर देते हैं। सुग्रीव को अपना खोया राज्य और परिवार वापिस मिल गया। भगवान की उदारता में कमी नहीं, पर उसे पाने के लिए घण्टी हिला देना भर काफी नहीं। सदुद्देश्यों के लिए बढ़-चढ़कर त्याग बलिदान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
मनुष्य की चालाकी में कमी नहीं। उनका वश चले तो उनके निवास और परिवार को भी बेच खायें। पर भक्त ऐसा नहीं कर सकते। सुग्रीव के सभी साथी सहचर समुद्र पर पुल बनाने और लंका का दमन करने के लिए निहत्थे होते हुए भी गये थे। नल-नील ने इंजीनियर का कौशल दिखाया था। बेचारी गिलहरी तक बालों में बालू भरकर समुद्र पाटने के लिए पहुंची थी। उसने राम की हथेली पर बैठकर दुलार भरा वह प्यार पाया जिसके लिए तथाकथित योगी-यती तरसते ही रहते हैं। भगवान का दर्शन पाने की जिन्हें सचमुच ललक है, उन्हें गिलहरी जैसा पुरुषार्थ और जटायु जैसा अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, चाहे प्राण भले ही देने पड़ें। घायल जटायु को भगवान ने अपने आंसुओं से स्नान कराया था। जो इस झंझट से बचकर पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराने पर सम्पदाओं की गठरी लूटना चाहते हैं, उन्हें उनकी क्षुद्रता उस स्थान तक पहुंचने ही नहीं देती, जहां वे पहुंचना चाहते हैं।
हनुमान का समर्पण सर्वविदित है। राम का पक्ष न्याय का था और रावण का अन्याय का। धर्म की रक्षा और अधर्म का उन्मूलन करना ही अवतार का और उसके अनुयायियों का कर्तव्य है। इसमें चाहे निजी हानि कितनी ही होती हो, कठिनाई कितनी ही उठानी पड़ती हो। हनुमान ने यही किया। वे किसी व्यक्ति विशेष के दास या चाकर नहीं थे, उन्होंने नीति को विजयी बनाने के लिए लंका दहन, संजीवनी पर्वत उखाड़ने से लेकर अनेकानेक कष्ट सहे, पर क्या वे घाटे में रहे? सुग्रीव के यहां साधारण सेवक की तरह कार्य करने का बन्धन छूटा और वे देवताओं की गणना में गिने गये। राम पंचायत में छठे सदस्य बने और संसार भर में पूजे गये। जितने मन्दिर राम के हैं उससे कहीं अधिक हनुमान के हैं। उन्हें जो बल, पराक्रम, विवेक, कौशल, यश प्राप्त हुआ वह सब उस भक्ति का प्रतिफल था जो सच्चे अर्थों में कर्तव्य परायणता और उदार साहसिकता से भरी-पूरी थी।
निषादराज की कथा प्रख्यात है। राम मिलन के लिए सेना समेत भरत के सम्बन्ध में उसने समझा कि वे लोग राम को मारकर निष्कंटक राज करने जा रहे हैं। निषाद ने भरत की सारी सेना को गंगा में डुबा देने की तैयारी कर ली। पीछे वस्तुस्थिति विदित होने पर डुबोने की अपेक्षा खर्चीले आतिथ्य की व्यवस्था सीमित साधनों उसने की। भक्ति इसी को कहते हैं, जिसमें अनीति से लड़ना और नीति का समर्थन करना होता है।
शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाये थे, पर वह सुयोग बना तब जब उस भीलनी ने मातंग ऋषि के आश्रम का समीपवर्ती रास्ता साफ बनाये रखने का व्रत वर्षों निबाहा था। अर्जुन के घोड़े भगवान ने चलाये, वे सारथी बने, पर कदम उठा तब जब दैन्य, हीनता का भाव मिटाकर विशाल भारत बनाने की योजना कार्यान्वित करने के लिए वह तैयार हुआ। बलि के द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने पहुंचे थे ताकि पृथ्वी पर सुव्यवस्था का अवसर मिल सके। द्रौपदी को उन्होंने लाज बचाने हेतु वस्त्र इसलिये दिया था कि वह इससे पूर्व एक सन्त को वस्त्रहीन देखकर अपनी आधी साड़ी फाड़कर दान दे चुकी थी। भगवान दानी तो अवश्य हैं। एक बीज के बदले हर वर्ष हजारों फूल, फल, बीज देते हैं। पर यह होता तभी है जब आरम्भ में एक बीज अपने को मिट्टी में मिलाकर गला देने के लिए तैयार होता है। भक्ति और उसके वरदान मिलने की बात इसी प्रकार सोची जा सकती है। मीरा को विष के प्याले और सर्पों के पिटारे से इसलिए बचाया था कि वह राणा के भयंकर प्रतिबन्धों की चिन्ता न करते हुए गांव-गांव, घर-घर भक्ति का अमृत बांटने के लिए प्रचार यात्रा पर निकल पड़ी थी।
वीरपुर (गुजरात) के बापा जलाराम को भगवान ने दर्शन भी दिए और अखण्ड अन्नपूर्णा भण्डार वाली झोली दी थी, किन्तु यह अनुग्रह पाने से पहले जलाराम यह व्रत निभाते रहे थे कि वे दिन भर खेत में काम करेंगे और पत्नी सत्पात्रों को तब तक भोजन पकाती-खिलाती रहेगी जब तक घर में अनाज रहे। भगवान उदार तो हैं पर उन्हीं के लिए जो प्रामाणिकता और उदारता की कसौटी पर खरे सिद्ध हो सके। छल करने वालों के लिए उनका ‘‘छलिया’’ नाम भी प्रसिद्ध है। दुष्टों के दमन में उनका ‘‘रुद्र’’ रूप ही परिलक्षित होता है।
भगवान का दृश्य और प्रत्यक्ष रूप विराट ब्रह्म ही है, जिसे अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकमुशुण्डि जी आदि ने देखा था। इसे विश्व उद्यान या जनता जनार्दन भी कह सकते हैं। लोक सेवा के रूप में भक्ति की यथार्थता का परिचय जिस प्रकार दिया जा सकता है उतना और किसी प्रकार नहीं।
सुदामा के पैर धोकर भगवान ने पिये थे। भृगु की लात सीने पर खाई थी। यह ब्राह्मण की गरिमा को अपने से बड़ी बताने के उद्देश्य से भगवान ने किया था। ब्राह्मण वे हैं, जो गृहस्थी संभालते हुए क्षेत्रीय सेवा साधना की योजना में संलग्न रहते हैं और अपना निर्वाह अपरिग्रही की तरह करते हैं। साधु, ब्राह्मण वर्ग का वह पक्ष है जो विरक्त वानप्रस्थ रहकर परिव्राजक की तरह अलख जगाता—वायु की तरह प्राण संजोता और बादलों की तरह सद्-विचारों का अमृत बरसाता है। इस वर्ग को श्रेष्ठ, पूज्य और भगवान के अधिक समीप इसलिए माना गया है कि वे भगवान के परमार्थ परक प्रयोजनों में निरन्तर लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ साधन को सर्वथा भुलाये रहते हैं।
भगवान की भक्ति में घटा उन्हें पड़ता है जो पूजा पाठ का दाना बिखेर कर चिड़ियों की तरह देवी-देवताओं को बहकाने-फंसाने में लगे रहते हैं। किन्तु जिन्हें सेवा धर्म प्रिय है, जो लोक सेवा को भगवान का अविच्छिन्न अंग मानते हैं, वे जितना बोते हैं, उससे अनेक गुना पाते हैं। मक्का का एक बोया हुआ दाना हजारों मक्का के दानों का समुच्चय बनकर वापस लौटता है। इसी प्रकार भक्ति का वास्तविक स्वरूप यदि सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के रूप में चरितार्थ किया जाय तो भक्त भगवान के प्राणप्रिय बनते हैं। नारद कभी-कभी विष्णु लोक जा पहुंचते थे। यह छूट उन्हें इसलिए मिली थी कि वे भक्ति प्रचार के लिए, धर्म विस्तार के लिए निरन्तर भ्रमण करते रहते थे। ढाई घड़ी से अधिक एक स्थान पर खड़े न होते थे। भगवान बुद्ध को मनुष्य होते हुए भी भगवान कहलाने का श्रेय इसलिए मिला कि संसार में फैले हुए अभाव को मिटाने और सर्वत्र धर्मचक्र प्रवर्तन की प्रक्रिया गतिशील करने के लिए अपने को उन्होंने पूर्णतः समर्पित कर दिया था। सेवाभावी जहां समाज का नेतृत्व करता है, वहां प्रत्यक्ष और परोक्ष इतने लाभ पाता है जो त्याग की तुलना में हजारों गुने अधिक होते हैं।
आगे बढ़े तो पाया :
जीव की मूल सत्ता शुक्राणु के रूप में इतनी छोटी होती है कि आंख से देखी भी नहीं जा सकती, किन्तु भ्रूण में प्रवेश करने के बाद माता की शरीर सम्पदा उसे मिलने लगती है और नौ महीने में वह इस योग्य हो जाता है कि बाह्य संसार में प्रवेश कर सके। इसके बाद भी माता दूध पिलाने, खिलाने, पहिनाने, सफाई रखने जैसी अनेकों सुरक्षात्मक सावधानियां रखती है। यदि ऐसा न करे, तो बालक का जीवित रह सकना संभव नहीं। अब पिता की बारी आती है। पोषण, शिक्षण, स्वावलम्बन, विवाह आदि के लिए वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग खर्च करता है और सभ्य-शिक्षित बनाने में योगदान देता है। इन सहायताओं के बल पर मनुष्य आगे बढ़ता है। यदि उसे उपरोक्त सभी प्रसंगों में अपने पैरों खड़े होना पड़े, तो वह क्या कुछ बन सकेगा? इस सम्बन्ध में असमंजस और सन्देह ही बना रहेगा।
सुसभ्य छत्रछाया में सभी को विकसित होने का असाधारण अवसर मिलता है। चतुर माली बगीचे को ऐसा नयनाभिराम और लाभदायक बना देता है, उसे देखकर दर्शकों तक को प्रशंसा करनी पड़ती है। सुव्यवस्थित गुरुकुलों में पढ़कर छात्र अत्यन्त मेधावी नर-रत्न बनकर निकलते रहे। यह कार्य कोई विद्यार्थी अपने आप पोथी पढ़कर सम्पन्न नहीं कर सकता है। पहलवान अखाड़ों में ही बना जाता है। अभिनेता बनने के लिए रंगमंच चाहिए। प्रगति के लिए आवश्यक वातावरण, मार्ग दर्शन एवं अनुदान—इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। स्व-उत्पादित तो जंगलों के झाड़-झंखाड़ ही होते अनगढ़ चट्टानें देव प्रतिमाओं का कलेवर धारण नहीं कर सकतीं, इसके लिए निर्माता कलाकार चाहिए। आभूषण भी हर कोई नहीं बना सकता। यह स्वर्णकार का ही कौशल है, जो अनगढ़ धातु खण्डों को अपनी कलाकारिता से ऐसे आभूषणों में बदल देता है, जिससे सिर और गले तक की शोभा बढ़ती है, नाक-कान तक सजते हैं, उंगली के पोरवे भी।
व्यक्ति की भौतिक अथवा आत्मिक प्रगति के लिए किसी सहायक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। गायक, वादक, मूर्तिकार, चित्रकार आदि को किसी न किसी निष्णात के यहां शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। आत्मिक क्षेत्र में तो यह एक प्रकार से अनिवार्य है, नितान्त आवश्यक। जिस प्रकार भ्रूण बिन्दु को माता का रस-रक्त चाहिए उसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए ऐसे संरक्षक परिपोषक की आवश्यकता पड़ती है जो अपने विषय का पूर्ण पारंगत भी हो और साथ ही उतना उदार भी कि अपनी उपार्जित सम्पदा को बिना संकोच के ‘इच्छुक’ को उदारतापूर्वक हस्तांतरित करता रहे।
चर्चा गुरु-शिष्य संयोग-सुयोग की हो रही है। उसमें प्रमुखता एवं वरिष्ठता गुरु की ही है, क्योंकि वह अपने विषय का धनी भी होता है और दानी भी। इतिहास साक्षी है कि जहां कहीं, जब कभी कोई महत्वपूर्ण प्रसंग सामने आया है, तब उसमें गुरु की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका अपना चमत्कार प्रस्तुत करती दिखाई दी है। यों भटकते-पूछते भी पथिक देर-सवेर में ठिकाने तक जा पहुंचते हैं, पर उन्हें वह सुगमता और सफलता नहीं मिलती, जो गुरु और शिष्य का संयोग बनने पर संभव होती है। इस तथ्य को समझते हुए निराश एकलव्य को द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिट्टी से बनानी पड़ी थी। श्रद्धा के बल पर उसने उस खिलौने को असली द्रोणाचार्य से कहीं अधिक सुयोग्य एवं सहायक शिक्षक बना लिया था।
विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के बहाने राम-लक्ष्मण को अपने तपोवन में ले गये थे। वहां उन्हें बला और अतिबला गायत्री और सावित्री की रहस्यमयी जानकारी दी थी। फलतः सीता स्वयंवर जीतने, लंका विजय करने, राम राज्य की प्रतिष्ठा करने एवं भगवान कहे जाने की स्थिति तक वे पहुंचे थे। ऐसा सुयोग भरत, शत्रुघन को नहीं मिला था। उन्हें सामान्य स्थिति में रहना पड़ा। वे विश्व विख्यात न बन सके।
नारद के परामर्श से भगीरथ गंगावतरण में प्रवृत्त हुए थे। उन्हीं का निर्देशन परशुराम को मिला था कि संव्याप्त अनीति के धुर्रे बिखेर दें। वे परामर्श मात्र देकर चले नहीं गये थे, वरन् आदि से अन्त तक उनकी साज-संभाल करते और कठिनाइयों का समाधान करते रहे थे। नचिकेता ने यमाचार्य से पंचाग्नि विद्यायें प्राप्त की थीं और वे उस आधार पर ऊर्जा विज्ञान की समग्रता एवं प्रवीणता उपलब्ध कर सके थे। गुरुकुल की महत्ता इसी दृष्टि से थी कि वहां पुस्तकें ही नहीं पढ़ाई जाती थीं, वरन् छात्र में नये प्राण फूंकने और तुच्छ से महान बनाने की प्रक्रिया भी सम्पन्न की जाती थी।
भारतीय संस्कृति की पुण्य परमात्मा में माता-पिता के अतिरिक्त संरक्षकों की तीसरी पदवी गुरु की है। यही प्रत्यक्ष त्रिदेव हैं। शिव के बिना जिस प्रकार देव समुच्चय अधूरा रहता है, उसी प्रकार उच्चस्तरीय शिक्षार्थी भी उपयुक्त गुरु के अभाव में अनाथ-अपंग की स्थिति में पड़ा रहता है। अभाव, अज्ञान एवं अशक्ति से ऊफनते इस भवसागर जैसे महानद को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए जिस मजबूत पतवार वाले जहाज की जरूरत है, उसे ही गुरु कहा गया है।
महानता के पुरातन इतिहास में गुरु गरिमा की जितनी बड़ी भूमिका रही है, उतनी किसी ओर की नहीं। इसलिए भावनाशील शिक्षार्थी गुरु दक्षिणा में आचार्य को मुंहमांगा अनुदान अपनी समूची सामर्थ्य को भी न्यौछावर करते हुए हर संभावना को साकार कर दिखाते थे। हरिश्चन्द्र ने अपना राजपाट ही नहीं, शरीर और परिवार तक इस गुरु दक्षिणा के निमित्त समर्पित कर दिया था। वाजिश्रवा, हरिश्चन्द्र और बिम्बसार की भी ऐसी ही कथायें हैं। जो पाया था, उसका मूल्य चुकाते समय इन भावनाशील शिष्यों ने कृपणता का परिचय नहीं दिया। आरुणि, उद्दालक, सत्यकेतु और द्रुपद की कथायें सुप्रसिद्ध हैं और उनके गुरु ने अनुदानों को देखते हुए शिष्यों के लिए उपयुक्त प्रतिदान प्रस्तुत करने में भी कोताही नहीं की थी।
कुछ ही शताब्दियों के बीच घटित हुई घटनाओं में कई ऐसी हैं जो रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन करती हैं। भगवान बुद्ध ने अपने तपोबल से अनेकों को भागीदार बनाया और उनसे बड़े काम कराये। कुमारजीव को उन्होंने समूचे चीन का धर्मगुरु बना दिया। मंचूरिया, मंगोलिया, कोरिया, जापान तक में वह दूसरा बुद्ध माना जाने लगा था। तथागत का कार्यक्रम एक केन्द्र से धर्मचक्र प्रवर्तन की धुरी घुमाना था। वे स्वयं समूचे संसार और एशिया में किस प्रकार भ्रमण करते? उन्होंने अंगुलिमाल, अम्बपाली जैसों का कायाकल्प किया और उनके द्वारा पूर्वी-दक्षिणी एशिया में नवीन चेतना जगाई। एक दुर्दान्त डाकू उच्चकोटि का धर्म प्रचारक बन गया और अनेकों की पर्यंक शायिनी नर्तकी अम्बपाली ने सुविस्तृत क्षेत्र के नारी समुदाय में ऐसा प्राण फूंका मानो किसी ने उस तपती जमीन पर अमृत बरसा दिया हो। वह देवी में बदल गयी, साध्वी हो गयी। क्या यह पतित समझा जाने वाला परिकर बिना गुरु-कृपा के ऐसी स्थिति में पहुंच सकता था कि उनके चरणों पर कोटि-कोटि जन-समुदाय के पलक-पांवड़े बिछे। बिम्बसार ने राज्यकोष बौद्ध विहार बनाने में चुका दिया और हर्षवर्धन ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का समूचा भार उठाया। लगता है कि इस शिष्यों को घाटे में रहना पड़ा, पर उस घाटे पर कुबेर जैसे रत्न-भण्डारों को न्यौछावर किया जा सकता है, जिसने मनुष्यों को देवताओं से बढ़कर सम्माननीय बना दिया। कोटि-कोटि कण्ठों से गदगद कण्ठ में जिनकी यशोगाथा गाई गयी। ऐसा सौभाग्य क्या किसी छोटी-मोटी धनराशि और सुख-सम्पदा से लाखों गुना बढ़-चढ़कर नहीं है? बुद्ध के अवतार होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनने सामान्य स्तर के लोगों को लाखों की संख्या में महामानवों की पंक्ति में बिठाया। समर्थ गुरु के अभाव में यह लाखों भिक्षुओं और भिक्षुणियों की धर्म सेवा विश्वमानस का नवनिर्माण करने के लिए निकल न पाती।
तपस्वी चाणक्य की तप सम्पदा गाय के दूध भरे थनों की तरह निःसृत हो रही थी, पर प्रश्न यह था कि सत्पात्र खोजे बिना यह अमृत किस पर लुटाया जाय। आखिर चंद्रगुप्त मिल गया। एक क्षुद्र जाति के बालक को राजपूतों के बीच वरिष्ठता कैसे मिलती? पर चाणक्य की योजना, दक्षता और तप सम्पदा थी जिसे लेकर चंद्रगुप्त भारत के गौरव में चार चांद लगा देने में समर्थ हुआ। यह मिला तब था जब उसने अपने पराक्रम का लाभ अपने निज के लिए नहीं, समस्त राष्ट्र के लिए अर्पित करने का व्रत लिया और आश्वासन दिया था।
समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी की ऐसी ही गाथायें हैं। गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने गुरु को अपना निजत्व पूरी तरह समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी तप साधना विश्व संस्कृति में नई हलचल पैदा करने के लिए प्रदान की और शिष्य ने अनुभव किया कि उनके प्राण और शरीर में गुरु ही काम कर रहा है। उनने संसार भर में रामकृष्ण मिशन मठों की स्थापना की निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर विवेकानन्द नाम की कुटिया भी कहीं नहीं बनायी।
महायोगी और उद्भट विद्वान विरजानन्द की पाठशाला में ढेरों विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते थे और पढ़ाई पूरी करके कथा बांचने, जन्मपत्री बनाने का धन्धा करते थे। गुरु को आवश्यकता ऐसे शिष्य की थी जो पेट पालने और मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद न मांगकर अपने को देश, धर्म, समाज और संस्कृति के लिए समर्पित करे। अगणित छात्र आये और चले गये, पर एक छात्र मिला—दयानन्द, जिसने आचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा और जब उन्होंने तन, मन, धन पाखण्ड खण्डन करने के निमित्त समर्पित करने की मांग की तो शिष्य ने गुरु आदेश के लिये सर्वस्व समर्पित कर दिया। वे ब्रह्मचारी से संन्यासी बन गये और जब तक जिए, एक निष्ठ भाव से वेद धर्म का प्रचार करने में लगे रहे। आर्य समाज के रूप में उनका दिवंगत शरीर अभी भी जीवित है। उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के—समाज सुधार अभियान के रूप में स्मरण किया जाता है।
ऊपर की पंक्तियों में कुछ ऐसे नेतृत्व करने वाले शिष्यों का उल्लेख है जिन्होंने पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनने की दिशा में कदम बढ़ाये और असंख्यों के हृदय पटलों पर अपने आसन जमाये।
आज ऐसे ही नेताओं का, शिष्यों का आह्वान हो रहा है जिन्हें विपुल सहायता प्रदान करने के लिए देव सत्ता व्याकुल है। तलाशा उन्हें जा रहा है जो इस अनुदान को पाकर अपने को और धर्म परम्परा को धन्य बनावें। खोजना गुरु को नहीं, शिष्यों को इस तरह पड़ रहा है मानो भारत माता की बहुमूल्य रत्न-राशि कहीं मिट्ठी धूलि में गुम हो गई हो।
यह तथ्य याद रखा जाना चाहिए कि टंकी में पानी जब तक भरा रहता है, तब तक उसके साथ जुड़े हुए नल का प्रवाह चलता ही रहता है। बिजली घर के साथ जुड़े हुए बल्ब, पंखे, मोटर गतिशील रहते ही हैं। समर्थ गुरुसत्ता के साथ जो जुड़ सके, उसे थकने, हारने या निराश होने की कोई जरूरत नहीं। नेतृत्व के शिक्षार्थी किसी प्रकार हताश न हों, अपने आपको समर्थता के साथ जोड़े रहने का संकल्प भर सुदृढ़ बनाये रहें।
युग नेतृत्व के उदाहरणों की शृंखला में निकटवर्ती, अभी तक जीवित व्यक्तियों को तलाशना हो तो प्रज्ञा अभियान के सूत्र-संचालक को उलट-पुलट कर परखा जा सकता है। उनने ऐसे अनेक काम किए हैं जिनसे असम्भव शब्द को संभव में बदलने की नेपोलियन वाली उक्ति को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। यह हाड़ मांस से बनी काया के व्यक्तित्व का कर्तृत्व नहीं हो सकता। मनुष्य की कार्यक्षमता सीमित है, कौशल और साधन भी सीमित हैं, पर असीम साधनों की आवश्यकता पड़े और वे सभी यथासमय जुटते चले जायें तो एक शब्द में यही कहना होगा कि यह किसी दैवी शक्ति का पृष्ठ पोषण है। इसके उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रमाणों से हर एक यही कहता है कि इस प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष भूमिका गुरुतत्व की है।
एक लाख ‘नेता’ सच्चे अर्थों में नेता विनिर्मित करने का संकल्प इतना भारी है जिसे तराजू के पलड़े में रखने के बाद दूसरे में पुरातन काल के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को रखते हुए बराबरी की बात सोचनी पड़ेगी। क्या यह सब हो सकेगा? क्या यह सम्भव है? क्या एक लाख युग शिल्पी नव सृजन में संलग्न होकर सतयुग की वापिसी का वह प्रयोजन पूरा कर सकेंगे जिसे समुद्र सेतु बांधने के समतुल्य माना जा सके। बात अचम्भे की है, पर तब-तब सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य से इतने बड़े उत्तरदायित्व को तौला जाय। जब स्थिति ऐसी हो कि प्रस्तुत संकल्प की प्रेरणा, निर्धारणा, योजना ही नहीं, उसकी सफलता की जिम्मेदारी भी किसी महान शक्ति ने उठाई हो तो उसकी सफलता में किसी प्रकार का सन्देह या असमंजस करने की गुंजायश नहीं है। इस अवसर को लाभ उठाने पर वही उक्ति लागू होगी जिसमें कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ‘‘शत्रु को मैंने पहले ही मार कर रख दिया है, तुझे तो विजय का श्रेय भर लूटना है।’’
यथार्थता की कसौटी पर कसे जाने के उपरान्त स्पष्ट होता है कि भगवान का दरबार ‘‘अन्धेर नगरी-बेबूझ राजा’’ की उक्ति चरितार्थ नहीं करता। वहां उन्हीं को अनुकम्पा का अनुदान मिलता है, जिन्हें प्रामाणिकता और उदारता की कसौटी पर खरा कस लिया जाता है। भक्ति का सीधा अर्थ होता है—सेवा अर्थात् लोक मंगल। यह उन्हीं से बन पड़ता है, जो अपने को हर दृष्टि से संयम की आग में तपाते हैं। औसत नागरिक का जीवन जीकर उससे ऐसा कुछ बचा लेते हैं जिसे समयदान, अंशदान के रूप में दरिद्र नारायण के चरणों पर अर्पित किया जा सके। सत्प्रवृत्ति संवर्धन में उसका बढ़ा-चढ़ा उपयोग किया जा सके। सच्चे भगवद्-भक्त इसी स्तर के होते रहे हैं और बदले में आत्म संतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह का प्रत्यक्ष प्रतिफल उपलब्ध करते रहे हैं।
सुदामा का उदाहरण सामने है। उनका विशालकाय गुरुकुल था। सुयोग्य अध्यापन और वातावरण जहां भी होगा, वहां छात्रों की कमी न रहेगी। पुरातन काल में गुरुकुल-विश्वविद्यालय ही छात्रों के शिक्षण और निर्वाह की दुहरी व्यवस्था वहन करते थे, पर उस क्षेत्र में उदारचेताओं की कमी पड़ जाने से गुरुकुलों के ऊपर भारी आर्थिक कठिनाई लदी रहने लगी। आसरा किसका लिया जाय। सोचा गया कि भगवान को पकड़ा जाय। वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने स्थिति को जाना और अपनी सम्पदा कुटुम्बियों के विलास हेतु छोड़ने की अपेक्षा यह उचित समझा कि जो पास में है वह सब कुछ उच्च आदर्श के हेतु विसर्जित कर दिया जाय। द्वारिकापुरी की सारी सम्पदा उठकर सुदामापुरी चली आयी। लक्ष्मीनारायण की अनुकम्पा ऐसों को ही प्राप्त होती है। जेबकटी का रास्ता अपनाने वालों को नहीं।
भक्तों में एक आते हैं—विभीषण। उनने अनीति में सगे भाई का भी साथ नहीं दिया। अपमान और अभाव सहते रहे और समय आने पर अपनी समूची वफादारी उस न्याय और नीति के पक्ष में समर्पित कर दी, जिसे प्रकारान्तर से भगवान कहते हैं। भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। उसे सोने की लंका और अद्वितीय विदुषी मन्दोदरी का लाभ मिला। ऐसे ही प्रसंग सिद्ध करते हैं कि भगवान भक्त-वत्सल और विभूतियों के अधिपति हैं।
सच्चे भक्तों की श्रेणी में सुग्रीव का नाम आता है। राम के साथ अनीति हुई। दुष्टों ने सीताहरण कर लिया। खोजने के लिए दूतों और लड़ने के लिए सैनिकों की आवश्यकता हुई। भक्त सुग्रीव ने जो कुछ भी अपने पास था मुक्त हस्त से दिया। दानी की खाली हुई जेबें भगवान भर देते हैं। सुग्रीव को अपना खोया राज्य और परिवार वापिस मिल गया। भगवान की उदारता में कमी नहीं, पर उसे पाने के लिए घण्टी हिला देना भर काफी नहीं। सदुद्देश्यों के लिए बढ़-चढ़कर त्याग बलिदान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
मनुष्य की चालाकी में कमी नहीं। उनका वश चले तो उनके निवास और परिवार को भी बेच खायें। पर भक्त ऐसा नहीं कर सकते। सुग्रीव के सभी साथी सहचर समुद्र पर पुल बनाने और लंका का दमन करने के लिए निहत्थे होते हुए भी गये थे। नल-नील ने इंजीनियर का कौशल दिखाया था। बेचारी गिलहरी तक बालों में बालू भरकर समुद्र पाटने के लिए पहुंची थी। उसने राम की हथेली पर बैठकर दुलार भरा वह प्यार पाया जिसके लिए तथाकथित योगी-यती तरसते ही रहते हैं। भगवान का दर्शन पाने की जिन्हें सचमुच ललक है, उन्हें गिलहरी जैसा पुरुषार्थ और जटायु जैसा अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, चाहे प्राण भले ही देने पड़ें। घायल जटायु को भगवान ने अपने आंसुओं से स्नान कराया था। जो इस झंझट से बचकर पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराने पर सम्पदाओं की गठरी लूटना चाहते हैं, उन्हें उनकी क्षुद्रता उस स्थान तक पहुंचने ही नहीं देती, जहां वे पहुंचना चाहते हैं।
हनुमान का समर्पण सर्वविदित है। राम का पक्ष न्याय का था और रावण का अन्याय का। धर्म की रक्षा और अधर्म का उन्मूलन करना ही अवतार का और उसके अनुयायियों का कर्तव्य है। इसमें चाहे निजी हानि कितनी ही होती हो, कठिनाई कितनी ही उठानी पड़ती हो। हनुमान ने यही किया। वे किसी व्यक्ति विशेष के दास या चाकर नहीं थे, उन्होंने नीति को विजयी बनाने के लिए लंका दहन, संजीवनी पर्वत उखाड़ने से लेकर अनेकानेक कष्ट सहे, पर क्या वे घाटे में रहे? सुग्रीव के यहां साधारण सेवक की तरह कार्य करने का बन्धन छूटा और वे देवताओं की गणना में गिने गये। राम पंचायत में छठे सदस्य बने और संसार भर में पूजे गये। जितने मन्दिर राम के हैं उससे कहीं अधिक हनुमान के हैं। उन्हें जो बल, पराक्रम, विवेक, कौशल, यश प्राप्त हुआ वह सब उस भक्ति का प्रतिफल था जो सच्चे अर्थों में कर्तव्य परायणता और उदार साहसिकता से भरी-पूरी थी।
निषादराज की कथा प्रख्यात है। राम मिलन के लिए सेना समेत भरत के सम्बन्ध में उसने समझा कि वे लोग राम को मारकर निष्कंटक राज करने जा रहे हैं। निषाद ने भरत की सारी सेना को गंगा में डुबा देने की तैयारी कर ली। पीछे वस्तुस्थिति विदित होने पर डुबोने की अपेक्षा खर्चीले आतिथ्य की व्यवस्था सीमित साधनों उसने की। भक्ति इसी को कहते हैं, जिसमें अनीति से लड़ना और नीति का समर्थन करना होता है।
शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाये थे, पर वह सुयोग बना तब जब उस भीलनी ने मातंग ऋषि के आश्रम का समीपवर्ती रास्ता साफ बनाये रखने का व्रत वर्षों निबाहा था। अर्जुन के घोड़े भगवान ने चलाये, वे सारथी बने, पर कदम उठा तब जब दैन्य, हीनता का भाव मिटाकर विशाल भारत बनाने की योजना कार्यान्वित करने के लिए वह तैयार हुआ। बलि के द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने पहुंचे थे ताकि पृथ्वी पर सुव्यवस्था का अवसर मिल सके। द्रौपदी को उन्होंने लाज बचाने हेतु वस्त्र इसलिये दिया था कि वह इससे पूर्व एक सन्त को वस्त्रहीन देखकर अपनी आधी साड़ी फाड़कर दान दे चुकी थी। भगवान दानी तो अवश्य हैं। एक बीज के बदले हर वर्ष हजारों फूल, फल, बीज देते हैं। पर यह होता तभी है जब आरम्भ में एक बीज अपने को मिट्टी में मिलाकर गला देने के लिए तैयार होता है। भक्ति और उसके वरदान मिलने की बात इसी प्रकार सोची जा सकती है। मीरा को विष के प्याले और सर्पों के पिटारे से इसलिए बचाया था कि वह राणा के भयंकर प्रतिबन्धों की चिन्ता न करते हुए गांव-गांव, घर-घर भक्ति का अमृत बांटने के लिए प्रचार यात्रा पर निकल पड़ी थी।
वीरपुर (गुजरात) के बापा जलाराम को भगवान ने दर्शन भी दिए और अखण्ड अन्नपूर्णा भण्डार वाली झोली दी थी, किन्तु यह अनुग्रह पाने से पहले जलाराम यह व्रत निभाते रहे थे कि वे दिन भर खेत में काम करेंगे और पत्नी सत्पात्रों को तब तक भोजन पकाती-खिलाती रहेगी जब तक घर में अनाज रहे। भगवान उदार तो हैं पर उन्हीं के लिए जो प्रामाणिकता और उदारता की कसौटी पर खरे सिद्ध हो सके। छल करने वालों के लिए उनका ‘‘छलिया’’ नाम भी प्रसिद्ध है। दुष्टों के दमन में उनका ‘‘रुद्र’’ रूप ही परिलक्षित होता है।
भगवान का दृश्य और प्रत्यक्ष रूप विराट ब्रह्म ही है, जिसे अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकमुशुण्डि जी आदि ने देखा था। इसे विश्व उद्यान या जनता जनार्दन भी कह सकते हैं। लोक सेवा के रूप में भक्ति की यथार्थता का परिचय जिस प्रकार दिया जा सकता है उतना और किसी प्रकार नहीं।
सुदामा के पैर धोकर भगवान ने पिये थे। भृगु की लात सीने पर खाई थी। यह ब्राह्मण की गरिमा को अपने से बड़ी बताने के उद्देश्य से भगवान ने किया था। ब्राह्मण वे हैं, जो गृहस्थी संभालते हुए क्षेत्रीय सेवा साधना की योजना में संलग्न रहते हैं और अपना निर्वाह अपरिग्रही की तरह करते हैं। साधु, ब्राह्मण वर्ग का वह पक्ष है जो विरक्त वानप्रस्थ रहकर परिव्राजक की तरह अलख जगाता—वायु की तरह प्राण संजोता और बादलों की तरह सद्-विचारों का अमृत बरसाता है। इस वर्ग को श्रेष्ठ, पूज्य और भगवान के अधिक समीप इसलिए माना गया है कि वे भगवान के परमार्थ परक प्रयोजनों में निरन्तर लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ साधन को सर्वथा भुलाये रहते हैं।
भगवान की भक्ति में घटा उन्हें पड़ता है जो पूजा पाठ का दाना बिखेर कर चिड़ियों की तरह देवी-देवताओं को बहकाने-फंसाने में लगे रहते हैं। किन्तु जिन्हें सेवा धर्म प्रिय है, जो लोक सेवा को भगवान का अविच्छिन्न अंग मानते हैं, वे जितना बोते हैं, उससे अनेक गुना पाते हैं। मक्का का एक बोया हुआ दाना हजारों मक्का के दानों का समुच्चय बनकर वापस लौटता है। इसी प्रकार भक्ति का वास्तविक स्वरूप यदि सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के रूप में चरितार्थ किया जाय तो भक्त भगवान के प्राणप्रिय बनते हैं। नारद कभी-कभी विष्णु लोक जा पहुंचते थे। यह छूट उन्हें इसलिए मिली थी कि वे भक्ति प्रचार के लिए, धर्म विस्तार के लिए निरन्तर भ्रमण करते रहते थे। ढाई घड़ी से अधिक एक स्थान पर खड़े न होते थे। भगवान बुद्ध को मनुष्य होते हुए भी भगवान कहलाने का श्रेय इसलिए मिला कि संसार में फैले हुए अभाव को मिटाने और सर्वत्र धर्मचक्र प्रवर्तन की प्रक्रिया गतिशील करने के लिए अपने को उन्होंने पूर्णतः समर्पित कर दिया था। सेवाभावी जहां समाज का नेतृत्व करता है, वहां प्रत्यक्ष और परोक्ष इतने लाभ पाता है जो त्याग की तुलना में हजारों गुने अधिक होते हैं।
आगे बढ़े तो पाया :
जीव की मूल सत्ता शुक्राणु के रूप में इतनी छोटी होती है कि आंख से देखी भी नहीं जा सकती, किन्तु भ्रूण में प्रवेश करने के बाद माता की शरीर सम्पदा उसे मिलने लगती है और नौ महीने में वह इस योग्य हो जाता है कि बाह्य संसार में प्रवेश कर सके। इसके बाद भी माता दूध पिलाने, खिलाने, पहिनाने, सफाई रखने जैसी अनेकों सुरक्षात्मक सावधानियां रखती है। यदि ऐसा न करे, तो बालक का जीवित रह सकना संभव नहीं। अब पिता की बारी आती है। पोषण, शिक्षण, स्वावलम्बन, विवाह आदि के लिए वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग खर्च करता है और सभ्य-शिक्षित बनाने में योगदान देता है। इन सहायताओं के बल पर मनुष्य आगे बढ़ता है। यदि उसे उपरोक्त सभी प्रसंगों में अपने पैरों खड़े होना पड़े, तो वह क्या कुछ बन सकेगा? इस सम्बन्ध में असमंजस और सन्देह ही बना रहेगा।
सुसभ्य छत्रछाया में सभी को विकसित होने का असाधारण अवसर मिलता है। चतुर माली बगीचे को ऐसा नयनाभिराम और लाभदायक बना देता है, उसे देखकर दर्शकों तक को प्रशंसा करनी पड़ती है। सुव्यवस्थित गुरुकुलों में पढ़कर छात्र अत्यन्त मेधावी नर-रत्न बनकर निकलते रहे। यह कार्य कोई विद्यार्थी अपने आप पोथी पढ़कर सम्पन्न नहीं कर सकता है। पहलवान अखाड़ों में ही बना जाता है। अभिनेता बनने के लिए रंगमंच चाहिए। प्रगति के लिए आवश्यक वातावरण, मार्ग दर्शन एवं अनुदान—इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। स्व-उत्पादित तो जंगलों के झाड़-झंखाड़ ही होते अनगढ़ चट्टानें देव प्रतिमाओं का कलेवर धारण नहीं कर सकतीं, इसके लिए निर्माता कलाकार चाहिए। आभूषण भी हर कोई नहीं बना सकता। यह स्वर्णकार का ही कौशल है, जो अनगढ़ धातु खण्डों को अपनी कलाकारिता से ऐसे आभूषणों में बदल देता है, जिससे सिर और गले तक की शोभा बढ़ती है, नाक-कान तक सजते हैं, उंगली के पोरवे भी।
व्यक्ति की भौतिक अथवा आत्मिक प्रगति के लिए किसी सहायक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। गायक, वादक, मूर्तिकार, चित्रकार आदि को किसी न किसी निष्णात के यहां शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। आत्मिक क्षेत्र में तो यह एक प्रकार से अनिवार्य है, नितान्त आवश्यक। जिस प्रकार भ्रूण बिन्दु को माता का रस-रक्त चाहिए उसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए ऐसे संरक्षक परिपोषक की आवश्यकता पड़ती है जो अपने विषय का पूर्ण पारंगत भी हो और साथ ही उतना उदार भी कि अपनी उपार्जित सम्पदा को बिना संकोच के ‘इच्छुक’ को उदारतापूर्वक हस्तांतरित करता रहे।
चर्चा गुरु-शिष्य संयोग-सुयोग की हो रही है। उसमें प्रमुखता एवं वरिष्ठता गुरु की ही है, क्योंकि वह अपने विषय का धनी भी होता है और दानी भी। इतिहास साक्षी है कि जहां कहीं, जब कभी कोई महत्वपूर्ण प्रसंग सामने आया है, तब उसमें गुरु की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका अपना चमत्कार प्रस्तुत करती दिखाई दी है। यों भटकते-पूछते भी पथिक देर-सवेर में ठिकाने तक जा पहुंचते हैं, पर उन्हें वह सुगमता और सफलता नहीं मिलती, जो गुरु और शिष्य का संयोग बनने पर संभव होती है। इस तथ्य को समझते हुए निराश एकलव्य को द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिट्टी से बनानी पड़ी थी। श्रद्धा के बल पर उसने उस खिलौने को असली द्रोणाचार्य से कहीं अधिक सुयोग्य एवं सहायक शिक्षक बना लिया था।
विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के बहाने राम-लक्ष्मण को अपने तपोवन में ले गये थे। वहां उन्हें बला और अतिबला गायत्री और सावित्री की रहस्यमयी जानकारी दी थी। फलतः सीता स्वयंवर जीतने, लंका विजय करने, राम राज्य की प्रतिष्ठा करने एवं भगवान कहे जाने की स्थिति तक वे पहुंचे थे। ऐसा सुयोग भरत, शत्रुघन को नहीं मिला था। उन्हें सामान्य स्थिति में रहना पड़ा। वे विश्व विख्यात न बन सके।
नारद के परामर्श से भगीरथ गंगावतरण में प्रवृत्त हुए थे। उन्हीं का निर्देशन परशुराम को मिला था कि संव्याप्त अनीति के धुर्रे बिखेर दें। वे परामर्श मात्र देकर चले नहीं गये थे, वरन् आदि से अन्त तक उनकी साज-संभाल करते और कठिनाइयों का समाधान करते रहे थे। नचिकेता ने यमाचार्य से पंचाग्नि विद्यायें प्राप्त की थीं और वे उस आधार पर ऊर्जा विज्ञान की समग्रता एवं प्रवीणता उपलब्ध कर सके थे। गुरुकुल की महत्ता इसी दृष्टि से थी कि वहां पुस्तकें ही नहीं पढ़ाई जाती थीं, वरन् छात्र में नये प्राण फूंकने और तुच्छ से महान बनाने की प्रक्रिया भी सम्पन्न की जाती थी।
भारतीय संस्कृति की पुण्य परमात्मा में माता-पिता के अतिरिक्त संरक्षकों की तीसरी पदवी गुरु की है। यही प्रत्यक्ष त्रिदेव हैं। शिव के बिना जिस प्रकार देव समुच्चय अधूरा रहता है, उसी प्रकार उच्चस्तरीय शिक्षार्थी भी उपयुक्त गुरु के अभाव में अनाथ-अपंग की स्थिति में पड़ा रहता है। अभाव, अज्ञान एवं अशक्ति से ऊफनते इस भवसागर जैसे महानद को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए जिस मजबूत पतवार वाले जहाज की जरूरत है, उसे ही गुरु कहा गया है।
महानता के पुरातन इतिहास में गुरु गरिमा की जितनी बड़ी भूमिका रही है, उतनी किसी ओर की नहीं। इसलिए भावनाशील शिक्षार्थी गुरु दक्षिणा में आचार्य को मुंहमांगा अनुदान अपनी समूची सामर्थ्य को भी न्यौछावर करते हुए हर संभावना को साकार कर दिखाते थे। हरिश्चन्द्र ने अपना राजपाट ही नहीं, शरीर और परिवार तक इस गुरु दक्षिणा के निमित्त समर्पित कर दिया था। वाजिश्रवा, हरिश्चन्द्र और बिम्बसार की भी ऐसी ही कथायें हैं। जो पाया था, उसका मूल्य चुकाते समय इन भावनाशील शिष्यों ने कृपणता का परिचय नहीं दिया। आरुणि, उद्दालक, सत्यकेतु और द्रुपद की कथायें सुप्रसिद्ध हैं और उनके गुरु ने अनुदानों को देखते हुए शिष्यों के लिए उपयुक्त प्रतिदान प्रस्तुत करने में भी कोताही नहीं की थी।
कुछ ही शताब्दियों के बीच घटित हुई घटनाओं में कई ऐसी हैं जो रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन करती हैं। भगवान बुद्ध ने अपने तपोबल से अनेकों को भागीदार बनाया और उनसे बड़े काम कराये। कुमारजीव को उन्होंने समूचे चीन का धर्मगुरु बना दिया। मंचूरिया, मंगोलिया, कोरिया, जापान तक में वह दूसरा बुद्ध माना जाने लगा था। तथागत का कार्यक्रम एक केन्द्र से धर्मचक्र प्रवर्तन की धुरी घुमाना था। वे स्वयं समूचे संसार और एशिया में किस प्रकार भ्रमण करते? उन्होंने अंगुलिमाल, अम्बपाली जैसों का कायाकल्प किया और उनके द्वारा पूर्वी-दक्षिणी एशिया में नवीन चेतना जगाई। एक दुर्दान्त डाकू उच्चकोटि का धर्म प्रचारक बन गया और अनेकों की पर्यंक शायिनी नर्तकी अम्बपाली ने सुविस्तृत क्षेत्र के नारी समुदाय में ऐसा प्राण फूंका मानो किसी ने उस तपती जमीन पर अमृत बरसा दिया हो। वह देवी में बदल गयी, साध्वी हो गयी। क्या यह पतित समझा जाने वाला परिकर बिना गुरु-कृपा के ऐसी स्थिति में पहुंच सकता था कि उनके चरणों पर कोटि-कोटि जन-समुदाय के पलक-पांवड़े बिछे। बिम्बसार ने राज्यकोष बौद्ध विहार बनाने में चुका दिया और हर्षवर्धन ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का समूचा भार उठाया। लगता है कि इस शिष्यों को घाटे में रहना पड़ा, पर उस घाटे पर कुबेर जैसे रत्न-भण्डारों को न्यौछावर किया जा सकता है, जिसने मनुष्यों को देवताओं से बढ़कर सम्माननीय बना दिया। कोटि-कोटि कण्ठों से गदगद कण्ठ में जिनकी यशोगाथा गाई गयी। ऐसा सौभाग्य क्या किसी छोटी-मोटी धनराशि और सुख-सम्पदा से लाखों गुना बढ़-चढ़कर नहीं है? बुद्ध के अवतार होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनने सामान्य स्तर के लोगों को लाखों की संख्या में महामानवों की पंक्ति में बिठाया। समर्थ गुरु के अभाव में यह लाखों भिक्षुओं और भिक्षुणियों की धर्म सेवा विश्वमानस का नवनिर्माण करने के लिए निकल न पाती।
तपस्वी चाणक्य की तप सम्पदा गाय के दूध भरे थनों की तरह निःसृत हो रही थी, पर प्रश्न यह था कि सत्पात्र खोजे बिना यह अमृत किस पर लुटाया जाय। आखिर चंद्रगुप्त मिल गया। एक क्षुद्र जाति के बालक को राजपूतों के बीच वरिष्ठता कैसे मिलती? पर चाणक्य की योजना, दक्षता और तप सम्पदा थी जिसे लेकर चंद्रगुप्त भारत के गौरव में चार चांद लगा देने में समर्थ हुआ। यह मिला तब था जब उसने अपने पराक्रम का लाभ अपने निज के लिए नहीं, समस्त राष्ट्र के लिए अर्पित करने का व्रत लिया और आश्वासन दिया था।
समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी की ऐसी ही गाथायें हैं। गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने गुरु को अपना निजत्व पूरी तरह समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी तप साधना विश्व संस्कृति में नई हलचल पैदा करने के लिए प्रदान की और शिष्य ने अनुभव किया कि उनके प्राण और शरीर में गुरु ही काम कर रहा है। उनने संसार भर में रामकृष्ण मिशन मठों की स्थापना की निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर विवेकानन्द नाम की कुटिया भी कहीं नहीं बनायी।
महायोगी और उद्भट विद्वान विरजानन्द की पाठशाला में ढेरों विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते थे और पढ़ाई पूरी करके कथा बांचने, जन्मपत्री बनाने का धन्धा करते थे। गुरु को आवश्यकता ऐसे शिष्य की थी जो पेट पालने और मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद न मांगकर अपने को देश, धर्म, समाज और संस्कृति के लिए समर्पित करे। अगणित छात्र आये और चले गये, पर एक छात्र मिला—दयानन्द, जिसने आचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा और जब उन्होंने तन, मन, धन पाखण्ड खण्डन करने के निमित्त समर्पित करने की मांग की तो शिष्य ने गुरु आदेश के लिये सर्वस्व समर्पित कर दिया। वे ब्रह्मचारी से संन्यासी बन गये और जब तक जिए, एक निष्ठ भाव से वेद धर्म का प्रचार करने में लगे रहे। आर्य समाज के रूप में उनका दिवंगत शरीर अभी भी जीवित है। उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के—समाज सुधार अभियान के रूप में स्मरण किया जाता है।
ऊपर की पंक्तियों में कुछ ऐसे नेतृत्व करने वाले शिष्यों का उल्लेख है जिन्होंने पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनने की दिशा में कदम बढ़ाये और असंख्यों के हृदय पटलों पर अपने आसन जमाये।
आज ऐसे ही नेताओं का, शिष्यों का आह्वान हो रहा है जिन्हें विपुल सहायता प्रदान करने के लिए देव सत्ता व्याकुल है। तलाशा उन्हें जा रहा है जो इस अनुदान को पाकर अपने को और धर्म परम्परा को धन्य बनावें। खोजना गुरु को नहीं, शिष्यों को इस तरह पड़ रहा है मानो भारत माता की बहुमूल्य रत्न-राशि कहीं मिट्ठी धूलि में गुम हो गई हो।
यह तथ्य याद रखा जाना चाहिए कि टंकी में पानी जब तक भरा रहता है, तब तक उसके साथ जुड़े हुए नल का प्रवाह चलता ही रहता है। बिजली घर के साथ जुड़े हुए बल्ब, पंखे, मोटर गतिशील रहते ही हैं। समर्थ गुरुसत्ता के साथ जो जुड़ सके, उसे थकने, हारने या निराश होने की कोई जरूरत नहीं। नेतृत्व के शिक्षार्थी किसी प्रकार हताश न हों, अपने आपको समर्थता के साथ जोड़े रहने का संकल्प भर सुदृढ़ बनाये रहें।
युग नेतृत्व के उदाहरणों की शृंखला में निकटवर्ती, अभी तक जीवित व्यक्तियों को तलाशना हो तो प्रज्ञा अभियान के सूत्र-संचालक को उलट-पुलट कर परखा जा सकता है। उनने ऐसे अनेक काम किए हैं जिनसे असम्भव शब्द को संभव में बदलने की नेपोलियन वाली उक्ति को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। यह हाड़ मांस से बनी काया के व्यक्तित्व का कर्तृत्व नहीं हो सकता। मनुष्य की कार्यक्षमता सीमित है, कौशल और साधन भी सीमित हैं, पर असीम साधनों की आवश्यकता पड़े और वे सभी यथासमय जुटते चले जायें तो एक शब्द में यही कहना होगा कि यह किसी दैवी शक्ति का पृष्ठ पोषण है। इसके उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रमाणों से हर एक यही कहता है कि इस प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष भूमिका गुरुतत्व की है।
एक लाख ‘नेता’ सच्चे अर्थों में नेता विनिर्मित करने का संकल्प इतना भारी है जिसे तराजू के पलड़े में रखने के बाद दूसरे में पुरातन काल के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को रखते हुए बराबरी की बात सोचनी पड़ेगी। क्या यह सब हो सकेगा? क्या यह सम्भव है? क्या एक लाख युग शिल्पी नव सृजन में संलग्न होकर सतयुग की वापिसी का वह प्रयोजन पूरा कर सकेंगे जिसे समुद्र सेतु बांधने के समतुल्य माना जा सके। बात अचम्भे की है, पर तब-तब सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य से इतने बड़े उत्तरदायित्व को तौला जाय। जब स्थिति ऐसी हो कि प्रस्तुत संकल्प की प्रेरणा, निर्धारणा, योजना ही नहीं, उसकी सफलता की जिम्मेदारी भी किसी महान शक्ति ने उठाई हो तो उसकी सफलता में किसी प्रकार का सन्देह या असमंजस करने की गुंजायश नहीं है। इस अवसर को लाभ उठाने पर वही उक्ति लागू होगी जिसमें कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ‘‘शत्रु को मैंने पहले ही मार कर रख दिया है, तुझे तो विजय का श्रेय भर लूटना है।’’