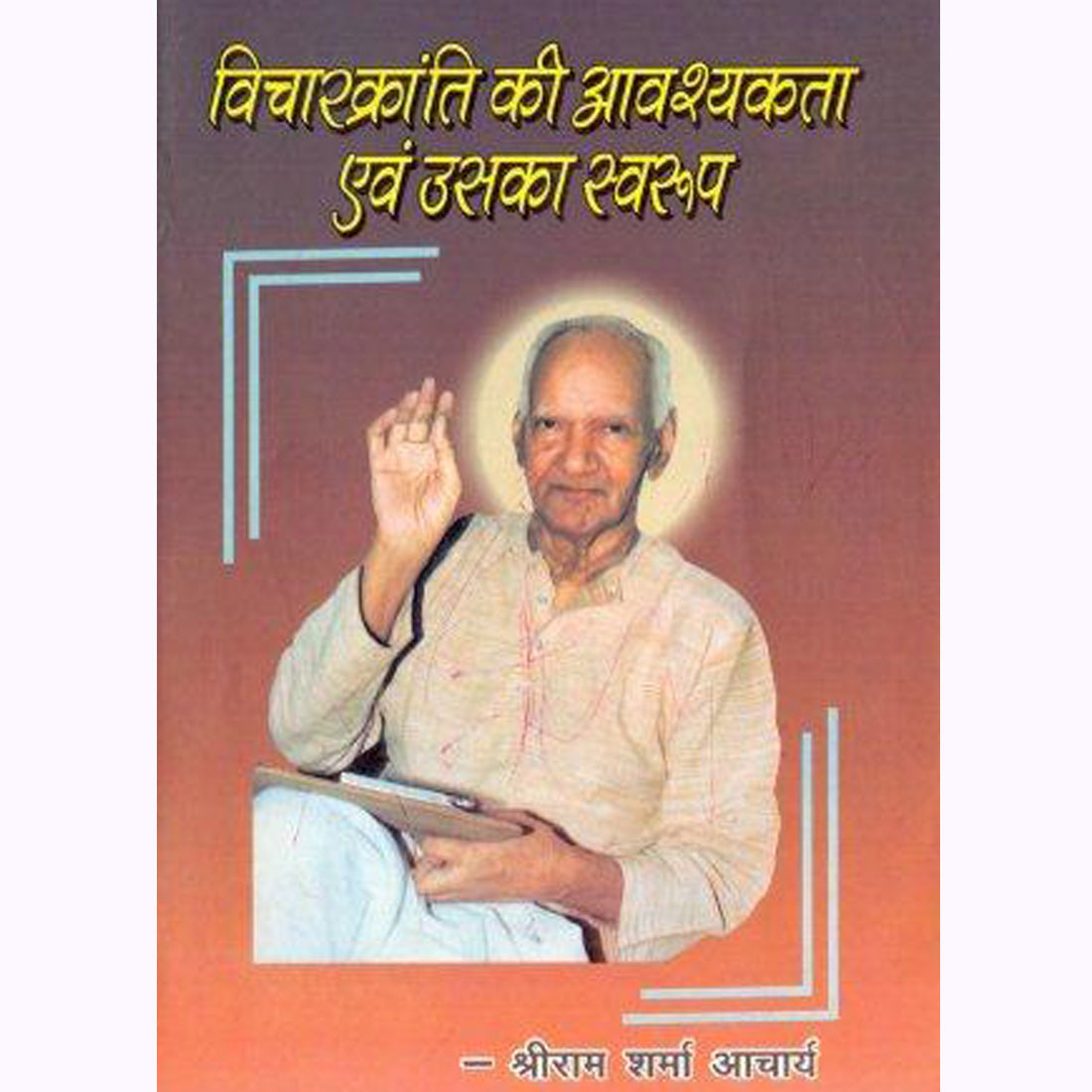विचारक्रान्ति की आवश्यकता एवं उसका स्वरूप 
नैतिक एवं बौद्धिक परिवर्तन का आह्वान
Read Scan Version
नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्रों में घुसी हुई भ्रान्तियां अपने-अपने क्षेत्रों में चित्र-विचित्र प्रथा परम्परा बनकर रही हैं और प्रचलन में इतनी गुंथ गई हैं कि उनकी अनुपयुक्तता के बारे में सन्देह करने तक की आवश्यकता नहीं समझी जाती।
मानवी सत्ता, स्रष्टा की अनुपम कलाकृति है उसे इसलिए सृजा गया है कि अपनी विशिष्टता और वरिष्ठता के सहारे इस विश्व उद्यान को सुरभित, समुन्नत रखे। औसत नागरिक की तरह सादगी भरा निर्वाह करे— उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श चरित्र की गौरव गरिमा बनाये रहे—पवित्रता एवं प्रखरता पर आधारित व्यक्तित्व समर्थ रखे—तथा ऐसी योजना बनाकर चले जिसका अनुकरण करने वाले निरन्तर ऊंचे उठते आगे बढ़ते रहें। संक्षेप में यही है मनुष्य की नीति मर्यादा का सार संक्षेप। इसका जो जितना परिपालन करता है वह उतना ही नीतिवान है। इस निर्धारण को जो जितना तोड़ता है जो लोभ, मोह और अहंकार के लिए ही मरता खपता है—जिसे वासना तृष्णा के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं—जिसे संकीर्ण स्वार्थ परता के आगे की बात सोचने की फुरसत ही नहीं—जिसके मन में लोक मंगल के उत्तरदायित्व निभाने के लिए उल्लास उठता ही नहीं उसे अनैतिक कहना चाहिए। उद्धत अपराधों की तरह संकीर्ण स्वार्थपरता भी तत्वदर्शियों द्वारा अनीति ही मानी गई है। देखा जाना चाहिए कि अनीति के व्यक्तिगत रुझान और सामुदायिक प्रचलन में कितनी गहरी जड़ें जमाई हैं। उन्हें उखाड़ने के लिए उतनी ही गहरी खुदाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। हर व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए कि प्रस्तुत प्रवाह में बहने पर वह किस प्रकार हर दृष्टि से घाटे ही घाटे में रहता है। समझना होगा कि यदि आदर्श वादिता अपनाई जा सके तो उसमें पूरी तरह लाभ ही लाभ है।
बौद्धिक क्षेत्र में अन्ध-विश्वासों के उलूकों ने कितने घोंसले बना रखे हैं और वे कितनी निश्चिन्तता पूर्वक बस गये हैं यह देखकर आश्चर्य होता है। आहार को ही लें भुना तला, मिर्च मसाले वाला स्वादिष्ट समझा जाने वाला अभक्ष्य ही हम सब उदरस्थ करते हैं। नशे पीते हैं। यह भूलते ही जा रहे हैं कि मानवी आहार में शाक−भाजी की प्रमुखता कितनी आवश्यक है। अन्न लेना हो तो उबाल लेना ही पर्याप्त है। मांस मानवी आहार में किसी दृष्टि से फिट नहीं बैठता। खरी नमक—सोडियम क्लोराइड—एक प्रकार का विष है। इसी प्रकार शीरा निचोड़ देने के बाद चीनी भी मीठा जहर सिद्ध होती है। पर कौन किसे समझाये कि वर्तमान पाक विद्या एवं स्वाद लिप्सा प्रकारांतर से धीमी आत्म हत्या ही सिद्ध होती है। यदि आहार क्षेत्र में विचार क्रान्ति का समावेश हो सके तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्रस्तुत दुर्बलता और रुग्णता से आधा छुटकारा अनायास ही मिल सकता है। इसी प्रकार सोने जागने, श्रम करने, धूप, हवा के सम्पर्क में रहने, ब्रह्मचर्य पालने जैसे मोटे-मोटे प्रकृति निर्देशों को पाला जा सके तो मनुष्य भी अन्य स्वच्छन्द जीवन जीने वाले प्राणियों की तरह निरोग एवं दीर्घजीवी रह सकता है। यदि आहार-विहार का प्रचलित प्रवाह उलटा जा सके तो समझना चाहिए कि पीड़ा सहने, चिकित्सा में धन गंवाने, अशक्त रहने, अनुपयोगी बनने, कुसमय बेमौत मरने जैसे अगणित संकटों से सहज छुटकारा मिल गया।
मानसिक विक्षोभों का प्रधान कारण है—निषेधात्मक चिन्तन। जो उपलब्ध है उसका सन्तोष आनन्द लेने की अपेक्षा जो नहीं है उसी की सूची बनाये फिरना, अधिक सम्पन्नों के साथ तुलना करके दरिद्र अनुभव करना। तुलना करनी ही है तो पिछड़ों के साथ अपने सौभाग्य को सराहा क्यों न जाए? चारों ओर जो उत्साहवर्धक भरा पड़ा है जिसे देखने, सोचने, स्मरण करने से कृतज्ञता, प्रसन्नता की अनुभूति होती है उसी पर ध्यान केन्द्रित क्यों न किया जाय? मनोकामनाओं के पर्वत शिर पर लादने की अपेक्षा निर्वाह में सन्तोष करने की आदत क्यों न डाली जाय। अभीष्ट प्रतिफल की ललक में आकुल-व्याकुल रहने की अपेक्षा कर्तव्यपालन में निरत रहने और उतने भर में गर्व−गौरव अनुभव करने की आदत क्यों न डाली जाय? हार-जीत की परवाह न करते हुए भी खिलाड़ी जब प्रसन्नतापूर्वक खेल का आनन्द ले सकते हैं तो जीवन नाटक में आने वाले उतार-चढ़ावों में अपना ही सन्तुलन क्यों बिगाड़ा जाय? हर कोई हमारी मर्जी पर चले इसका आग्रह क्यों हो? अपनी जैसी विचार स्वतन्त्रता दूसरों को क्यों न अपनाने दी जाय? आदि प्रश्न ऐसे हैं जिन पर यदि ठंडे मन से विचार किया जा सके और चिन्तन के अभ्यस्त ढर्रे में विवेक युक्त परिवर्तन किया जा सके तो तनाव, खीज, चिन्ता, आशंका, आवेश जैसे कितने ही मनोविकारों द्वारा निरन्तर झुलसते रहना समाप्त हो सकता है।
हंसने-हंसाने की हल्की-फुल्की चिन्तन प्रक्रिया एक आदत भर है जिस का अनुकूलता या प्रतिकूलता से कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है। मस्तिष्क सभी को उपलब्ध है। भाव सम्वेदना से भरा-पूरा अन्तःकरण किसके पास नहीं है। उस क्षीर सागर, कैलाश जैसे पुण्य क्षेत्र में भ्रष्टता और दुष्टता से सने कषाय-कल्मष भर लेने का ही परिणाम है कि ऋषि कल्प संभावनाओं वाली देवात्मा चेतना निकृष्ट नारकीयता में आबद्ध होकर रह जाती है। इसे उलटना हर विवेकशील के लिए सम्भव है। बाल्मीकि, अंगुलिमाल, बिल्वमंगल जैसे जब दृष्टिकोण बदलते ही कुछ से कुछ हो सकते हैं तो अन्य किसी के लिए वैसा आत्म परिवर्तन क्या कठिन हो सकता है।
परिवार एक भला-चंगा उद्यान है। उसे स्रष्टा की अमानत समझकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह सुसंस्कृत स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न चले। पत्नी के साथ मित्र, साथी भर मानकर चला जाय। यौनाचार की अति करके उस के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को क्षत-विक्षत न किया जाय। अनावश्यक प्रजनन से हर किसी के लिए सिर दर्द उत्पन्न न किया जाय। लड़की-लड़के में भेदभाव करने की कुटिलता से बचा जाय, हर सदस्य के प्रति एक आंख प्यार की और दूसरी सुधार की रखी जाय तो वह भ्रष्टाचार न पनपेगा जिस में प्रसन्नता करने के लिए अनुचित उपहार देने की रीति-नीति अपनाई जाती है। उत्तराधिकारियों के स्वावलम्बी होते हुए उन्हें पूर्वजों की सम्पत्ति मिले यह कानून प्रचलन चोरों ने चोरों के लिए ही बनाया है। हर समर्थ व्यक्ति को अपनी कमाई खानी चाहिये। पूर्वजों का छोड़ा धन, सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन में लगना चाहिये। आलस्य, प्रमाद, विलास, अपव्यय, उपेक्षा, असहयोग के विष वृक्ष यदि परिवार के खेत में न पनपने दिये जांय तो कोई कारण नहीं कि अपने इन्हीं घर-घरौंदों को नर-रत्नों की खदान के रूप में परिणत न किया जा सके। नये परिवार बनते और पुराने टूटे जा रहे हैं। खण्डहरों और मरघटों का विस्तार हो रहा है। ऐसी दशा में परिवारों को भटियारों की सराय तथा भेड़ों के बाड़े जैसा कुरुचिपूर्ण देखा पाया जा रहा है तो आश्चर्य ही क्या है।
शरीर, मस्तिष्क, परिवार की तरह ही अर्थ व्यवस्था का भी जीवन तन्त्र पर भारी प्रभाव पड़ता है। आज हर धनी-निर्धन हर किसी की आर्थिक आवश्यकता बढ़ी-चढ़ी है और तंगी अनुभव होती है। संचय और अपव्यय के लिए तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ता है। अनीति उपार्जन, अपराध, ऋण, रिश्वत, बेईमानी का दौर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर चलता है। इस कमी की पूर्ति उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह कि लोग चाहते हैं। लोभ-लिप्सा को न पटने वाली खाई और न बुझने वाली आग कहा गया है। रावण, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर, सिकन्दर जैसे धनाध्यक्षों का जब वैभव के पहाड़ हाथ लगने पर भी सन्तोष न मिला तो सामान्य स्तर वालों की बात ही क्या है। ऐसी दशा में अर्थ सन्तुलन बिठाने के लिए दृष्टिकोण परिवर्तन का नया आधार अपनाना पड़ेगा। औसत देशवासियों के स्तर का निर्वाह—तेते पांव पसारिये जितनी लम्बी सौर, सादा जीवन उच्च विचार वाले, विलास और अपव्यय में कटौती जैसे दूरदर्शितापूर्ण सिद्धान्त अपना लेने पर इस सम्बन्ध की समस्यायें सहज ही हल हो जाती हैं। आलस्य प्रमाद छोड़ा, श्रमशील बना, काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न माना और योग्यता वृद्धि में उत्साह रखा जाय तो स्तर के अनुरूप आजीविका बढ़ भी सकती है। प्रश्न विस्तार से कम, सदुपयोग से अधिक सम्बन्धित है। थोड़े से साधनों का भी यदि श्रेष्ठतम सदुपयोग बन पड़े तो गरीबी में भी अमीरों से बढ़कर आनन्द के साथ दिया जा सकता है। परिश्रम और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर उपार्जन और उपयोग का संतुलन बिठाया जाय तो अर्थसंकट इस तरह किसी को भी न सताये। जैसा कि अपव्ययी, दुर्व्यसनी और सामाजिक कुरीतियों की मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित लोगों को निरन्तर भुगतना पड़ता है।
इच्छित सम्पदा उपलब्ध कराने के लिए गढ़ा खजाना, लाटरी का नम्बर लक्ष्मी सिद्धि, ठगी, चोरी के फेर में पड़े रहने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि सोचने का तरीका उलट दिया जाय और सामर्थ्य भर कमाने, आवश्यकता भर खर्चने की सुसन्तुलित नीति अपनाई जाय। अध्यात्मवादी और साम्यवादी दोनों इस निर्धारण पर समान रूप से सहमत हैं। लिप्सा और तृष्णा को नियन्त्रित किया जा सके तो निर्वाह में औचित्य की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बचत को सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन में लगाया जा सके तो उतने भर से दरिद्रता का युग समाप्त हो सकता है और सीमित साधनों से हर दिशा में हर्ष उल्लास बरस सकता है।
शिक्षितों का सन्तोष देखते ही बनता है। कुछ एक को छोड़कर अधिकांश को बेकारी या अल्प आजीविका की शिकायत है। हर कोई ठाट-बाट की नौकरी चाहता है। श्रम कम से कम, आजीविका अधिक से अधिक आमतौर से शिक्षितों पर यही भूत चढ़ा रहता है। सभी को ऐसी ही ठाट-बाट की नौकरियां चाहिये। वे सभी को मिलें कैसे? उन्हें रखे कौन? अभी तो देश में शिक्षा मात्र 30 प्रतिशत है। अब अधिकांश शिक्षित होंगे और सभी ठाट-बाट की नौकरी मांगेंगे तब उनका मनोरथ पूरा होने में और भी विग्रह उत्पन्न होगा। शिक्षा का लक्ष्य मात्र नौकरी ही है तो संकट और भी अधिक बढ़ेगा। फलतः उस वर्ग का असन्तोष विग्रह ऐसे संकट खड़े करेगा, जैसा कि बिना पढ़े रहने पर उत्पन्न न होते।
यहां शिक्षा की निन्दा नहीं की जा रही। न उसे अनुपयोगी बताया जा रहा है वरन् कहा यह जा रहा है कि सामान्य ज्ञान की मैट्रिक स्तर की जीवनोपयोगी प्रारम्भिक सर्वसुलभ हो। उसके बाद कालेज में प्रवेश करने से पूर्व हर अभिभावक अपने बच्चों का आजीविका लक्ष्य निश्चित करें। यह मान कर चलें कि नौकरी हर वर्ग के छात्रों में से कठिनाई से 10-2 प्रतिशत को मिलेगी, शेष को अन्य आधार अपनाकर अपने पैरों खड़ा होना होगा। जो भी धारा जिसे अनुकूल पड़े वह उस स्तर की औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करे। जिन्हें किसी विषय का विशेषज्ञ बनना हो वे उसमें पारंगत होने की दृष्टि से लम्बे अध्ययन की योजना बनायें इसमें हर्ज नहीं, पर भेड़िया धंसान की तरह नौकरी के लिए कालेज की खर्चीली पढ़ाई के लिए धकापेल मचाना सर्वथा अबुद्धिमत्तापूर्ण है। नई पीढ़ी के लिए सहकारी उद्योग के सहारे उत्पादन तन्त्र खड़े करने और उनमें कठोर श्रम करने के लिए उद्यत रहने की बात मस्तिष्क के हर कोने में बिठा दी जाय तो शिक्षितों के जिस घुटन में घुटते और अवांछनीय दिशा में चल पड़ने का जो संकट खड़ा है उससे छुटकारे का मार्ग मिल सकता है।
शिक्षा व्यवस्था बनाने वालों का उत्तरदायित्व है कि वे पिछले दिनों से चले आ रहे घपले को बन्द करें। असन्तोष उत्पन्न करने वाली शिक्षा पद्धति का बदलें और ऐसा कुछ पढ़ायें जिससे जीवनोपयोगी सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त आजीविका उपार्जन का भी पथ प्रशस्त होता हो। कोसने से नहीं, ढर्रे पर लुढ़कते रहने से भी नहीं। बात तब बनेगी जब छात्र, अभिभावक एवं शिक्षातन्त्र के निर्माता व्यावहारिक नीति अपनायें और पढ़ने-पढ़ाने का समूचा ढांचा नये सिरे से निर्धारित करें।
व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित समस्याओं में अब अध्यात्म दर्शन का, आस्तिकता, आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का मात्र भक्ति और कर्मयोग का क्षेत्र बना रहता है। बौद्धिकता का दायरा तो बहुत बड़ा है पर उसे स्वास्थ्य सन्तुलन, अर्थ परिवार के अतिरिक्त धर्म दर्शन को और जोड़कर जीवन साधना के पंचशीलों से समेटा जा सकता है। दर्शन क्षेत्र की मान्यताओं को कसौटी पर कसा जाना चाहिये कि वे मनुष्य को अधिक सुसंस्कृत, अधिक पराक्रमी, अधिक उदार समाजनिष्ठ बनने में किस हद तक सहयोग देती हैं। विभिन्न धर्म सम्प्रदाओं के अन्तर्गत अगणित मान्यताओं और परम्पराओं का ऐसा उलझा हुआ जाल-जंजाल है कि एक को सच ठहराते ही शेष सभी को झूठ ठहरना पड़ता है। एकात्मता की ओर ले चलने वाले नैतिक सत्र उनमें हैं तो पर, प्रत्यक्षतः ऐसी मान्यताओं और परम्पराओं का ही घटाटोप है जो एक दूसरे से तालमेल बिठाने में सर्वथा असमर्थ है। ऐसी दशा में किसी धर्म दर्शन को सर्वांश में मान्यता देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि उनमें जो भी प्रतिपादन व्यक्ति को पवित्र प्रखर बनाने में समर्थ हों, मनुष्य मात्र पर समान रूप से लागू होते हों, उन्हें अपनाया जाय और शेष का खण्डन-मण्डन करने की अपेक्षा उसे उपेक्षा से डाल दिया जाय।
देवता को मनुहार, उपहार के सहारे प्रसन्न करके बिना उपयुक्त मूल्य चुकाये, कुछ भी मनोरथ पूरा करा लेने की मान्यता का अन्त होना चाहिये। देवत्व का अवलम्बन अन्तराल में दिव्य प्रेरणायें उभारने की सम्वेदनात्मक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाय। पूजा-उपासना को आत्म परिष्कार की अध्यात्म विज्ञान सम्मत प्रणाली माना जाय। उतने भर से पाप दंड भुगतने से छुटकारा मिलने या कोई विलक्षण चमत्कार प्रकट होने जैसी बात कल्पनाओं को निरस्त किया जाय। कथा-पुराणों के सुनने-सुनाने से नहीं, उनमें वर्णित नीति भाव को हृदयंगम करने से बात बनती है। परम्परायें अनादि काल से समय समय पर बदलती रहती हैं और भविष्य में भी यह क्रम चलता रहेगा, इसलिए प्रथा प्रचलनों के सम्बन्ध में किसी को भी पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिये। नीति मर्यादाओं को छोड़कर सभी प्राचीन निर्धारणों को इसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए कि उनमें से कितने तर्क-तथ्य, प्रमाण के अतिरिक्त सामयिक समाधान से किस हद तक सहायक होते हैं। तत्वदर्शन की असंख्य परस्पर विरोधी धारायें और मान्यतायें प्रचलित हैं। इनमें सबको तो मान्यता नहीं दी जा सकती। विवेक के आधार पर उनकी परिणति को ध्यान में रखते हुए युग दर्शन को नया रूप मिलना चाहिये। बौद्धिक क्रान्ति का प्रयोजन इसी प्रकार पूरा होता है।
सामाजिक क्रान्ति में ऐसे प्रचलनों को निरस्त किया जाना चाहिए, जो विषमता, विघटन, अन्याय, अनौचित्य के पृष्ठ पोषक हैं। पारिस्परिक स्नेह, सौमजस् सहयोग का विस्तार करने वाली वसुधैव कुटुम्बकम् की, आत्मवत् सर्वभूतेषु की दृष्टि पोषक प्रथा प्रचलनों को ही मान्यता मिले और शेष को औचित्य की कसौटी पर खोटी सिद्ध होने पर कूड़ेदान में झाड़-बुहार फेंक दिया जाय।
अपने समाज में नर-नारी के मध्य बरती जाने वाली भेद नीति, जन्म जाति के आधार पर मानी जाने वाली ऊंच-नीच, शिक्षा व्यवसाय, मृतकभोज, बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी अगणित कुप्रथायें प्रचलित हैं। इनमें सब से भयंकर है विवाहोन्माद जिसमें गरीबों द्वारा अमीरों का स्वांग बनाकर अपने बर्तन, कपड़े गंवा बैठने की मूर्खता की जाती है। सभी जानते हैं कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। फिर भी बुद्धिमान और मूर्ख उस सर्वनाशी कुप्रथा को छाती से लगाये बैठे हैं। इन सभी कुप्रचलनों में भ्रान्ति और अनीति बेतरह गुथी हुई है पर परम्परा के नाम पर उन्हें अपनाया और सर्वनाश के पथ पर बढ़ते चला जा रहा है। यह दुर्बुद्धि रुकनी ही चाहिये। अपना समाज सहकारी सहायक बने। उसकी अभिनव संरचना में कौटुम्बिकता के शाश्वत सिद्धान्तों का समावेश किया जाय। न जाति लिंग की विषमता रहे और न आर्थिक दृष्टि से किसी को गरीब अमीर रहने दिया जाय। न कोई उद्धत अहंकारी धनाध्यक्ष बने न किसी को पिछड़ेपन की पीड़ा भर्त्सना सहन करनी पड़े। अपराध की गुंजाइश ही न रहे यदि कहीं कोई उपद्रव उभरे तो उसे लोकशक्ति द्वारा इस प्रकार दबोच दिया जाय कि दूसरों को वैसा करने का साहस ही शेष न रहे। मिल-बांटकर खाने और हिल-मिलकर रहने की समाज संरचना के अन्तर्गत ही मनुष्य को सुख-शान्ति से रहने का अवसर मिल सकता है।
पांच अरब मनुष्यों में पाई जाने वाली भ्रान्तियों, विकृतियों, दुष्प्रवृत्तियों से जूझना कठिन लगता भर है। युग मनीषा यदि उसे कर गुजरने के लिए तत्परता प्रकट करे तो सत्य में हजार हाथी का बल होता है उस उक्ति के अनुसार श्रेष्ठता का वातावरण भी इसी प्रकार बन सकता है जिस प्रकार कि मुट्ठी भर लोगों ने अग्रगामी होकर दुष्टता भरे प्रचलनों से लोक मानस को भ्रष्ट करके रख दिया है।
मानवी सत्ता, स्रष्टा की अनुपम कलाकृति है उसे इसलिए सृजा गया है कि अपनी विशिष्टता और वरिष्ठता के सहारे इस विश्व उद्यान को सुरभित, समुन्नत रखे। औसत नागरिक की तरह सादगी भरा निर्वाह करे— उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श चरित्र की गौरव गरिमा बनाये रहे—पवित्रता एवं प्रखरता पर आधारित व्यक्तित्व समर्थ रखे—तथा ऐसी योजना बनाकर चले जिसका अनुकरण करने वाले निरन्तर ऊंचे उठते आगे बढ़ते रहें। संक्षेप में यही है मनुष्य की नीति मर्यादा का सार संक्षेप। इसका जो जितना परिपालन करता है वह उतना ही नीतिवान है। इस निर्धारण को जो जितना तोड़ता है जो लोभ, मोह और अहंकार के लिए ही मरता खपता है—जिसे वासना तृष्णा के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं—जिसे संकीर्ण स्वार्थ परता के आगे की बात सोचने की फुरसत ही नहीं—जिसके मन में लोक मंगल के उत्तरदायित्व निभाने के लिए उल्लास उठता ही नहीं उसे अनैतिक कहना चाहिए। उद्धत अपराधों की तरह संकीर्ण स्वार्थपरता भी तत्वदर्शियों द्वारा अनीति ही मानी गई है। देखा जाना चाहिए कि अनीति के व्यक्तिगत रुझान और सामुदायिक प्रचलन में कितनी गहरी जड़ें जमाई हैं। उन्हें उखाड़ने के लिए उतनी ही गहरी खुदाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। हर व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए कि प्रस्तुत प्रवाह में बहने पर वह किस प्रकार हर दृष्टि से घाटे ही घाटे में रहता है। समझना होगा कि यदि आदर्श वादिता अपनाई जा सके तो उसमें पूरी तरह लाभ ही लाभ है।
बौद्धिक क्षेत्र में अन्ध-विश्वासों के उलूकों ने कितने घोंसले बना रखे हैं और वे कितनी निश्चिन्तता पूर्वक बस गये हैं यह देखकर आश्चर्य होता है। आहार को ही लें भुना तला, मिर्च मसाले वाला स्वादिष्ट समझा जाने वाला अभक्ष्य ही हम सब उदरस्थ करते हैं। नशे पीते हैं। यह भूलते ही जा रहे हैं कि मानवी आहार में शाक−भाजी की प्रमुखता कितनी आवश्यक है। अन्न लेना हो तो उबाल लेना ही पर्याप्त है। मांस मानवी आहार में किसी दृष्टि से फिट नहीं बैठता। खरी नमक—सोडियम क्लोराइड—एक प्रकार का विष है। इसी प्रकार शीरा निचोड़ देने के बाद चीनी भी मीठा जहर सिद्ध होती है। पर कौन किसे समझाये कि वर्तमान पाक विद्या एवं स्वाद लिप्सा प्रकारांतर से धीमी आत्म हत्या ही सिद्ध होती है। यदि आहार क्षेत्र में विचार क्रान्ति का समावेश हो सके तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्रस्तुत दुर्बलता और रुग्णता से आधा छुटकारा अनायास ही मिल सकता है। इसी प्रकार सोने जागने, श्रम करने, धूप, हवा के सम्पर्क में रहने, ब्रह्मचर्य पालने जैसे मोटे-मोटे प्रकृति निर्देशों को पाला जा सके तो मनुष्य भी अन्य स्वच्छन्द जीवन जीने वाले प्राणियों की तरह निरोग एवं दीर्घजीवी रह सकता है। यदि आहार-विहार का प्रचलित प्रवाह उलटा जा सके तो समझना चाहिए कि पीड़ा सहने, चिकित्सा में धन गंवाने, अशक्त रहने, अनुपयोगी बनने, कुसमय बेमौत मरने जैसे अगणित संकटों से सहज छुटकारा मिल गया।
मानसिक विक्षोभों का प्रधान कारण है—निषेधात्मक चिन्तन। जो उपलब्ध है उसका सन्तोष आनन्द लेने की अपेक्षा जो नहीं है उसी की सूची बनाये फिरना, अधिक सम्पन्नों के साथ तुलना करके दरिद्र अनुभव करना। तुलना करनी ही है तो पिछड़ों के साथ अपने सौभाग्य को सराहा क्यों न जाए? चारों ओर जो उत्साहवर्धक भरा पड़ा है जिसे देखने, सोचने, स्मरण करने से कृतज्ञता, प्रसन्नता की अनुभूति होती है उसी पर ध्यान केन्द्रित क्यों न किया जाय? मनोकामनाओं के पर्वत शिर पर लादने की अपेक्षा निर्वाह में सन्तोष करने की आदत क्यों न डाली जाय। अभीष्ट प्रतिफल की ललक में आकुल-व्याकुल रहने की अपेक्षा कर्तव्यपालन में निरत रहने और उतने भर में गर्व−गौरव अनुभव करने की आदत क्यों न डाली जाय? हार-जीत की परवाह न करते हुए भी खिलाड़ी जब प्रसन्नतापूर्वक खेल का आनन्द ले सकते हैं तो जीवन नाटक में आने वाले उतार-चढ़ावों में अपना ही सन्तुलन क्यों बिगाड़ा जाय? हर कोई हमारी मर्जी पर चले इसका आग्रह क्यों हो? अपनी जैसी विचार स्वतन्त्रता दूसरों को क्यों न अपनाने दी जाय? आदि प्रश्न ऐसे हैं जिन पर यदि ठंडे मन से विचार किया जा सके और चिन्तन के अभ्यस्त ढर्रे में विवेक युक्त परिवर्तन किया जा सके तो तनाव, खीज, चिन्ता, आशंका, आवेश जैसे कितने ही मनोविकारों द्वारा निरन्तर झुलसते रहना समाप्त हो सकता है।
हंसने-हंसाने की हल्की-फुल्की चिन्तन प्रक्रिया एक आदत भर है जिस का अनुकूलता या प्रतिकूलता से कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है। मस्तिष्क सभी को उपलब्ध है। भाव सम्वेदना से भरा-पूरा अन्तःकरण किसके पास नहीं है। उस क्षीर सागर, कैलाश जैसे पुण्य क्षेत्र में भ्रष्टता और दुष्टता से सने कषाय-कल्मष भर लेने का ही परिणाम है कि ऋषि कल्प संभावनाओं वाली देवात्मा चेतना निकृष्ट नारकीयता में आबद्ध होकर रह जाती है। इसे उलटना हर विवेकशील के लिए सम्भव है। बाल्मीकि, अंगुलिमाल, बिल्वमंगल जैसे जब दृष्टिकोण बदलते ही कुछ से कुछ हो सकते हैं तो अन्य किसी के लिए वैसा आत्म परिवर्तन क्या कठिन हो सकता है।
परिवार एक भला-चंगा उद्यान है। उसे स्रष्टा की अमानत समझकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह सुसंस्कृत स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न चले। पत्नी के साथ मित्र, साथी भर मानकर चला जाय। यौनाचार की अति करके उस के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को क्षत-विक्षत न किया जाय। अनावश्यक प्रजनन से हर किसी के लिए सिर दर्द उत्पन्न न किया जाय। लड़की-लड़के में भेदभाव करने की कुटिलता से बचा जाय, हर सदस्य के प्रति एक आंख प्यार की और दूसरी सुधार की रखी जाय तो वह भ्रष्टाचार न पनपेगा जिस में प्रसन्नता करने के लिए अनुचित उपहार देने की रीति-नीति अपनाई जाती है। उत्तराधिकारियों के स्वावलम्बी होते हुए उन्हें पूर्वजों की सम्पत्ति मिले यह कानून प्रचलन चोरों ने चोरों के लिए ही बनाया है। हर समर्थ व्यक्ति को अपनी कमाई खानी चाहिये। पूर्वजों का छोड़ा धन, सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन में लगना चाहिये। आलस्य, प्रमाद, विलास, अपव्यय, उपेक्षा, असहयोग के विष वृक्ष यदि परिवार के खेत में न पनपने दिये जांय तो कोई कारण नहीं कि अपने इन्हीं घर-घरौंदों को नर-रत्नों की खदान के रूप में परिणत न किया जा सके। नये परिवार बनते और पुराने टूटे जा रहे हैं। खण्डहरों और मरघटों का विस्तार हो रहा है। ऐसी दशा में परिवारों को भटियारों की सराय तथा भेड़ों के बाड़े जैसा कुरुचिपूर्ण देखा पाया जा रहा है तो आश्चर्य ही क्या है।
शरीर, मस्तिष्क, परिवार की तरह ही अर्थ व्यवस्था का भी जीवन तन्त्र पर भारी प्रभाव पड़ता है। आज हर धनी-निर्धन हर किसी की आर्थिक आवश्यकता बढ़ी-चढ़ी है और तंगी अनुभव होती है। संचय और अपव्यय के लिए तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ता है। अनीति उपार्जन, अपराध, ऋण, रिश्वत, बेईमानी का दौर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर चलता है। इस कमी की पूर्ति उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह कि लोग चाहते हैं। लोभ-लिप्सा को न पटने वाली खाई और न बुझने वाली आग कहा गया है। रावण, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर, सिकन्दर जैसे धनाध्यक्षों का जब वैभव के पहाड़ हाथ लगने पर भी सन्तोष न मिला तो सामान्य स्तर वालों की बात ही क्या है। ऐसी दशा में अर्थ सन्तुलन बिठाने के लिए दृष्टिकोण परिवर्तन का नया आधार अपनाना पड़ेगा। औसत देशवासियों के स्तर का निर्वाह—तेते पांव पसारिये जितनी लम्बी सौर, सादा जीवन उच्च विचार वाले, विलास और अपव्यय में कटौती जैसे दूरदर्शितापूर्ण सिद्धान्त अपना लेने पर इस सम्बन्ध की समस्यायें सहज ही हल हो जाती हैं। आलस्य प्रमाद छोड़ा, श्रमशील बना, काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न माना और योग्यता वृद्धि में उत्साह रखा जाय तो स्तर के अनुरूप आजीविका बढ़ भी सकती है। प्रश्न विस्तार से कम, सदुपयोग से अधिक सम्बन्धित है। थोड़े से साधनों का भी यदि श्रेष्ठतम सदुपयोग बन पड़े तो गरीबी में भी अमीरों से बढ़कर आनन्द के साथ दिया जा सकता है। परिश्रम और ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर उपार्जन और उपयोग का संतुलन बिठाया जाय तो अर्थसंकट इस तरह किसी को भी न सताये। जैसा कि अपव्ययी, दुर्व्यसनी और सामाजिक कुरीतियों की मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित लोगों को निरन्तर भुगतना पड़ता है।
इच्छित सम्पदा उपलब्ध कराने के लिए गढ़ा खजाना, लाटरी का नम्बर लक्ष्मी सिद्धि, ठगी, चोरी के फेर में पड़े रहने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि सोचने का तरीका उलट दिया जाय और सामर्थ्य भर कमाने, आवश्यकता भर खर्चने की सुसन्तुलित नीति अपनाई जाय। अध्यात्मवादी और साम्यवादी दोनों इस निर्धारण पर समान रूप से सहमत हैं। लिप्सा और तृष्णा को नियन्त्रित किया जा सके तो निर्वाह में औचित्य की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बचत को सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन में लगाया जा सके तो उतने भर से दरिद्रता का युग समाप्त हो सकता है और सीमित साधनों से हर दिशा में हर्ष उल्लास बरस सकता है।
शिक्षितों का सन्तोष देखते ही बनता है। कुछ एक को छोड़कर अधिकांश को बेकारी या अल्प आजीविका की शिकायत है। हर कोई ठाट-बाट की नौकरी चाहता है। श्रम कम से कम, आजीविका अधिक से अधिक आमतौर से शिक्षितों पर यही भूत चढ़ा रहता है। सभी को ऐसी ही ठाट-बाट की नौकरियां चाहिये। वे सभी को मिलें कैसे? उन्हें रखे कौन? अभी तो देश में शिक्षा मात्र 30 प्रतिशत है। अब अधिकांश शिक्षित होंगे और सभी ठाट-बाट की नौकरी मांगेंगे तब उनका मनोरथ पूरा होने में और भी विग्रह उत्पन्न होगा। शिक्षा का लक्ष्य मात्र नौकरी ही है तो संकट और भी अधिक बढ़ेगा। फलतः उस वर्ग का असन्तोष विग्रह ऐसे संकट खड़े करेगा, जैसा कि बिना पढ़े रहने पर उत्पन्न न होते।
यहां शिक्षा की निन्दा नहीं की जा रही। न उसे अनुपयोगी बताया जा रहा है वरन् कहा यह जा रहा है कि सामान्य ज्ञान की मैट्रिक स्तर की जीवनोपयोगी प्रारम्भिक सर्वसुलभ हो। उसके बाद कालेज में प्रवेश करने से पूर्व हर अभिभावक अपने बच्चों का आजीविका लक्ष्य निश्चित करें। यह मान कर चलें कि नौकरी हर वर्ग के छात्रों में से कठिनाई से 10-2 प्रतिशत को मिलेगी, शेष को अन्य आधार अपनाकर अपने पैरों खड़ा होना होगा। जो भी धारा जिसे अनुकूल पड़े वह उस स्तर की औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करे। जिन्हें किसी विषय का विशेषज्ञ बनना हो वे उसमें पारंगत होने की दृष्टि से लम्बे अध्ययन की योजना बनायें इसमें हर्ज नहीं, पर भेड़िया धंसान की तरह नौकरी के लिए कालेज की खर्चीली पढ़ाई के लिए धकापेल मचाना सर्वथा अबुद्धिमत्तापूर्ण है। नई पीढ़ी के लिए सहकारी उद्योग के सहारे उत्पादन तन्त्र खड़े करने और उनमें कठोर श्रम करने के लिए उद्यत रहने की बात मस्तिष्क के हर कोने में बिठा दी जाय तो शिक्षितों के जिस घुटन में घुटते और अवांछनीय दिशा में चल पड़ने का जो संकट खड़ा है उससे छुटकारे का मार्ग मिल सकता है।
शिक्षा व्यवस्था बनाने वालों का उत्तरदायित्व है कि वे पिछले दिनों से चले आ रहे घपले को बन्द करें। असन्तोष उत्पन्न करने वाली शिक्षा पद्धति का बदलें और ऐसा कुछ पढ़ायें जिससे जीवनोपयोगी सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त आजीविका उपार्जन का भी पथ प्रशस्त होता हो। कोसने से नहीं, ढर्रे पर लुढ़कते रहने से भी नहीं। बात तब बनेगी जब छात्र, अभिभावक एवं शिक्षातन्त्र के निर्माता व्यावहारिक नीति अपनायें और पढ़ने-पढ़ाने का समूचा ढांचा नये सिरे से निर्धारित करें।
व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित समस्याओं में अब अध्यात्म दर्शन का, आस्तिकता, आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का मात्र भक्ति और कर्मयोग का क्षेत्र बना रहता है। बौद्धिकता का दायरा तो बहुत बड़ा है पर उसे स्वास्थ्य सन्तुलन, अर्थ परिवार के अतिरिक्त धर्म दर्शन को और जोड़कर जीवन साधना के पंचशीलों से समेटा जा सकता है। दर्शन क्षेत्र की मान्यताओं को कसौटी पर कसा जाना चाहिये कि वे मनुष्य को अधिक सुसंस्कृत, अधिक पराक्रमी, अधिक उदार समाजनिष्ठ बनने में किस हद तक सहयोग देती हैं। विभिन्न धर्म सम्प्रदाओं के अन्तर्गत अगणित मान्यताओं और परम्पराओं का ऐसा उलझा हुआ जाल-जंजाल है कि एक को सच ठहराते ही शेष सभी को झूठ ठहरना पड़ता है। एकात्मता की ओर ले चलने वाले नैतिक सत्र उनमें हैं तो पर, प्रत्यक्षतः ऐसी मान्यताओं और परम्पराओं का ही घटाटोप है जो एक दूसरे से तालमेल बिठाने में सर्वथा असमर्थ है। ऐसी दशा में किसी धर्म दर्शन को सर्वांश में मान्यता देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि उनमें जो भी प्रतिपादन व्यक्ति को पवित्र प्रखर बनाने में समर्थ हों, मनुष्य मात्र पर समान रूप से लागू होते हों, उन्हें अपनाया जाय और शेष का खण्डन-मण्डन करने की अपेक्षा उसे उपेक्षा से डाल दिया जाय।
देवता को मनुहार, उपहार के सहारे प्रसन्न करके बिना उपयुक्त मूल्य चुकाये, कुछ भी मनोरथ पूरा करा लेने की मान्यता का अन्त होना चाहिये। देवत्व का अवलम्बन अन्तराल में दिव्य प्रेरणायें उभारने की सम्वेदनात्मक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाय। पूजा-उपासना को आत्म परिष्कार की अध्यात्म विज्ञान सम्मत प्रणाली माना जाय। उतने भर से पाप दंड भुगतने से छुटकारा मिलने या कोई विलक्षण चमत्कार प्रकट होने जैसी बात कल्पनाओं को निरस्त किया जाय। कथा-पुराणों के सुनने-सुनाने से नहीं, उनमें वर्णित नीति भाव को हृदयंगम करने से बात बनती है। परम्परायें अनादि काल से समय समय पर बदलती रहती हैं और भविष्य में भी यह क्रम चलता रहेगा, इसलिए प्रथा प्रचलनों के सम्बन्ध में किसी को भी पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिये। नीति मर्यादाओं को छोड़कर सभी प्राचीन निर्धारणों को इसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए कि उनमें से कितने तर्क-तथ्य, प्रमाण के अतिरिक्त सामयिक समाधान से किस हद तक सहायक होते हैं। तत्वदर्शन की असंख्य परस्पर विरोधी धारायें और मान्यतायें प्रचलित हैं। इनमें सबको तो मान्यता नहीं दी जा सकती। विवेक के आधार पर उनकी परिणति को ध्यान में रखते हुए युग दर्शन को नया रूप मिलना चाहिये। बौद्धिक क्रान्ति का प्रयोजन इसी प्रकार पूरा होता है।
सामाजिक क्रान्ति में ऐसे प्रचलनों को निरस्त किया जाना चाहिए, जो विषमता, विघटन, अन्याय, अनौचित्य के पृष्ठ पोषक हैं। पारिस्परिक स्नेह, सौमजस् सहयोग का विस्तार करने वाली वसुधैव कुटुम्बकम् की, आत्मवत् सर्वभूतेषु की दृष्टि पोषक प्रथा प्रचलनों को ही मान्यता मिले और शेष को औचित्य की कसौटी पर खोटी सिद्ध होने पर कूड़ेदान में झाड़-बुहार फेंक दिया जाय।
अपने समाज में नर-नारी के मध्य बरती जाने वाली भेद नीति, जन्म जाति के आधार पर मानी जाने वाली ऊंच-नीच, शिक्षा व्यवसाय, मृतकभोज, बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी अगणित कुप्रथायें प्रचलित हैं। इनमें सब से भयंकर है विवाहोन्माद जिसमें गरीबों द्वारा अमीरों का स्वांग बनाकर अपने बर्तन, कपड़े गंवा बैठने की मूर्खता की जाती है। सभी जानते हैं कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। फिर भी बुद्धिमान और मूर्ख उस सर्वनाशी कुप्रथा को छाती से लगाये बैठे हैं। इन सभी कुप्रचलनों में भ्रान्ति और अनीति बेतरह गुथी हुई है पर परम्परा के नाम पर उन्हें अपनाया और सर्वनाश के पथ पर बढ़ते चला जा रहा है। यह दुर्बुद्धि रुकनी ही चाहिये। अपना समाज सहकारी सहायक बने। उसकी अभिनव संरचना में कौटुम्बिकता के शाश्वत सिद्धान्तों का समावेश किया जाय। न जाति लिंग की विषमता रहे और न आर्थिक दृष्टि से किसी को गरीब अमीर रहने दिया जाय। न कोई उद्धत अहंकारी धनाध्यक्ष बने न किसी को पिछड़ेपन की पीड़ा भर्त्सना सहन करनी पड़े। अपराध की गुंजाइश ही न रहे यदि कहीं कोई उपद्रव उभरे तो उसे लोकशक्ति द्वारा इस प्रकार दबोच दिया जाय कि दूसरों को वैसा करने का साहस ही शेष न रहे। मिल-बांटकर खाने और हिल-मिलकर रहने की समाज संरचना के अन्तर्गत ही मनुष्य को सुख-शान्ति से रहने का अवसर मिल सकता है।
पांच अरब मनुष्यों में पाई जाने वाली भ्रान्तियों, विकृतियों, दुष्प्रवृत्तियों से जूझना कठिन लगता भर है। युग मनीषा यदि उसे कर गुजरने के लिए तत्परता प्रकट करे तो सत्य में हजार हाथी का बल होता है उस उक्ति के अनुसार श्रेष्ठता का वातावरण भी इसी प्रकार बन सकता है जिस प्रकार कि मुट्ठी भर लोगों ने अग्रगामी होकर दुष्टता भरे प्रचलनों से लोक मानस को भ्रष्ट करके रख दिया है।
Write Your Comments Here:
- प्रस्तुत संकटों का कारण एवं निवारण
- विचारों में क्रान्ति आए तो समस्याएं सुलझें
- नवयुग की पृष्ठभूमि और मूलभूत आधार
- क्रान्ति का सही अर्थ समझें
- नैतिक एवं बौद्धिक परिवर्तन का आह्वान
- बुद्धिवाद नीतिनिष्ठा का पक्षधर बने
- मानवीय संवेदनाओं को पोषण दें— रौंदे नहीं
- नवनिर्माण का उत्कृष्टतावादी जीवनदर्शन
- समय की विषम बेला में वरिष्ठों का दायित्व