जीवन देवता की साधना-आराधना 
त्रिविध भवबंधन एवं उनसे मुक्ति
Read Scan Version
साधना से तात्पर्य है- साध लेना, सधा लेना। पशु प्रशिक्षक यही करते हैं।
अनगढ़ एवं उच्छृंखल पशुओं को वे एक रीति- नीति सिखाते हैं, उनको अभ्यस्त
बनाते हैं और उस स्थिति तक पहुँचाते हैं, जिसमें उस असंस्कृत प्राणी को
उपयोगी समझा जा सके। उसके बढ़े हुए स्तर का मूल्यांकन हो सके। पालने वाला
अपने को लाभान्वित हुआ देख सके। सिखाने वाला भी अपने प्रयास की सार्थकता
देखते हुए प्रसन्न हो सके।
देखा यह जाता है कि भक्त भगवान् को साधता है। उसको मूर्ख समझते हुए उसकी गलतियाँ निकालता है। तरह- तरह के उलाहने देता है। साथ ही गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़कर, खींसें निपोरकर अपना- अपना अनुचित उल्लू सीधा करने के लिये जाल- जंजाल बुनता है। प्रशंसा के पुल बाँधता है। छिटपुट भेंट चढ़ाकर उसे फुसलाने का प्रयत्न करता है। समझा जाता है कि सामान्य लोगों से व्यावहारिक जगत में आदान- प्रदान के आधार पर ही लेन- देन चलता है, पर ईश्वर या देवता ऐसे हैं जिन्हें वाणी की वाचालता तथा शारीरिक- मानसिक उचक- मचक करने भर से वशवर्ती नहीं किया जा सकता है। यह दार्शनिक भूल मनुष्य को एक प्रकार से छिपा हुआ नास्तिक बना देती है। प्रकट नास्तिक वे हैं जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने पर उसकी मान्यता से इंकार कर देते हैं। दूसरे छिपे नास्तिक वे हैं जो उससे पक्षपात की, मुफ्त में लम्बी- चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते रहते हैं। मनुष्य विधि व्यवस्था को तोड़ता- छोड़ता रहता है, पर ईश्वर के लिये यह सम्भव नहीं कि अपनी बनाई कर्मफल व्यवस्था का उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिये उत्साहित करे। तथाकथित भक्त लोग ऐसी ही आशाएँ किया करते हैं। अन्ततः: उन्हें निराश ही होना पड़ता है। इस निराशा की खीज और थकान से वे या तो साधना- विधान को मिथ्या बताते हैं या ईश्वर के निष्ठुर होने की मान्यता बनाते हैं। कई पाखण्डी कुछ भी हस्तगत न होने पर भी प्रवंचना रचते हैं और नकटा सम्प्रदाय की तरह अपनी सिद्धि- सफलता का बखान करते हैं। आज का आस्तिकवाद इसी विडम्बना में फँसा हुआ है और वह लगभग नास्तिकवाद के स्तर पर जा पहुँचा है।
आवश्यकता हैं भ्रान्तियों से निकलने और यथार्थता को अपनाने की। इस दिशा में मान्यताओं को अग्रगामी बनाते हुए हमें सोचना होगा कि जीवन साधना ही आध्यात्मिक स्वस्थता और बलिष्ठता है। इसी के बदले प्रत्यक्ष जीवन में मरण की प्रतीक्षा किये बिना, स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि का रसास्वाद करते रहा जा सकता है। उन लाभों को हस्तगत किया जा सकता है, जिनका उल्लेख अध्यात्म विधा की महत्ता बताते हुए शास्त्रकारों ने विस्तारपूर्वक किया है। सच्चे सन्तों- भक्तों का इतिहास भी विद्यमान है। खोजने पर प्रतीत होता है कि पूजा- पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा है, पर उन्होंने जीवन साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण जागरूकता बरती। इसमें व्यक्तिक्रम नहीं आने दिया। न आदर्श की अवज्ञा की और न उपेक्षा बरती। भाव- संवेदनाओं में श्रद्धा, विचार बुद्धि में प्रज्ञा और लोक व्यवहार में शालीन सद्भावना की निष्ठा अपनाकर कोई भी सच्चे अर्थों में जीवन देवता का सच्चा साधक बन सकता है। उसका उपहार, वरदान भी उसे हाथों हाथ मिलता चला जाता है।
ऋषियों, मनीषियों, सन्त- सुधारकों और वातावरण में ऊर्जा उभार देने वाले महामानवों की अनेकानेक साक्षियाँ विश्व इतिहास में भरी पड़ी हैं। इनमें से प्रत्येक को हर कसौटी पर जाँच- परखकर देखा जा सकता है कि उनमें से हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ा है। इससे कम में किसी को भी न आत्मा की प्राप्ति हो सकी न परमात्मा की, न ऐसों का लोक बना, और न परलोक। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। स्वास्थ्य वास्तविक सुन्दरता है। ऊपर से स्वस्थ व्यक्ति को वस्त्राभूषणों से, प्रसाधन सामग्री से सजाया भी जा सकता है। इसे सोने में सुगन्ध का संयोग बन पड़ा माना जा सकता है। जीवन साधना समग्र स्वास्थ्य बनाने जैसी विधा है। उसके ऊपर पूजा- पाठ का श्रृंगार सजाया जाय तो शोभा और भी अधिक बढ़ेगी। इसमें सुरुचि तो है किन्तु यह नहीं माना जाना चाहिये कि मात्र श्रृंगार साधनों के सहारे किसी जीर्ण- जर्जर रुग्ण या मृत शरीर को सुन्दर बना दिया जाय तो प्रयोजन सध सकता है। इससे तो उलटा उपहास ही बढ़ता है। इसके विपरीत यदि कोई हृष्ट- पुष्ट पहलवान मात्र लँगोट पहनकर अखाड़े में उतरता है तो भी उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा- अर्चना के लिये कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चल जाता है।
अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है, जिससे शरीर का निर्वाह लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। ईश्वर के दरबार में पहुँचकर सीना तानकर यह कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिये सौंपी गई थी, उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया।
इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें तीन हैं। इन्हीं को रावण, कुम्भकरण, मेघनाथ कहा गया है। यह दैवी भागवत् के महिषासुर, मधुकैटभ, रक्तबीज हैं। ये प्राय: साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में जा गिरता है। पशु, प्रेत और पिशाच की जिन्दगी जीता है। नर- वानर और नर- पामर के रूप में इन्हीं के चंगुल में फँसे हुए लोगों को देखा जाता है। ये तीन हैं- लोभ मोह एवं अहंकार। वासना, तृष्णा और कुत्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है।
लोक विजय के लिये सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धान्त अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में सन्तोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। लालची के लिये अनीति अपनाये बिना तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं होता। जो व्यक्ति विलास में अधिक खर्च करता है, वह प्रकारान्तर से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिये मजबूर करता है। इसीलिये शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी, संग्रही, अपव्ययी की भी ऐसी निन्दा की गई है।
अधिक कमाया जा सकता है, पर उसमें से निजी निर्वाह में सीमित व्यय करके शेष बचत क गिरों को उठाने, उठों को उछालने और सत्प्रवृत्तियों के संवर्द्धन में लगाया जाना चाहिये। राजा जनक जैसे उदाहरणों की कमी नहीं। मितव्ययी अनेक दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचता है। ऐसी हविश उसे सताती नहीं जिसके लिये अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु- ब्राह्मणों की यही परम्परा रही है। सज्जनों की शालीनता भी उसी आधार पर फलती- फूलती रही है। जीवन साधना के उस प्रथम अवरोध ‘लोभ’ को नियन्त्रित कराने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिये।
मोह वस्तुओं से भी होता है और व्यक्तियों से भी। छोटे दायरे में आत्मीयता सीमाबद्ध करना ही मोह है। उसके रहते हृदय की विशालता चरितार्थ ही नहीं होती। अपना शरीर और परिवार ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। उन्हीं के लिये मरने- खपने के कुचक्र में फँसे रहना पड़ता है। ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के दो आत्मवादी सिद्धान्त हैं। इनमें से एक को भी ‘मोहग्रस्त’ कार्यान्वित नहीं कर सकता। इसलिये अपने में सबको और सबमें अपने को देखने की दृष्टि विकसित करना जीवन साधना के लिये आवश्यक माना गया है।
परिवार छोटे से छोटा रखा जाय। पूर्ववर्ती अभिभावकों, बड़ों और आश्रितों के ऋणों को चुकाने की ही व्यवस्था नहीं बन पाती तो नये अतिथियों को क्यों न्यौत बुलाया जाय? समय की विषमता को देखते हुए अनावश्यक बच्चे उत्पन्न कर परिवार का भार बढ़ाना परले सिरे की भूल है। समान विचारों का साथी- सहयोगी मिले तो विवाह करने में हर्ज नहीं, पर वह एक दूसरे की सहायता सेवा करते हुए प्रगतिपथ पर अग्रसर होने के लिये ही किया जाना चाहिये। जिन्हें सन्तान की बहुत ललक हो, वे निर्धनों के बच्चे पालने के लिये ले सकते हैं। परिवार को स्वावलम्बी और सुसंस्कारी बनाना पर्याप्त है। औलाद के लिये विपुल सम्पदा उत्तराधिकार में छोड़ मरने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिये। मुफ्त का माल किसी को भी हजम नहीं होता। वह दुर्बुद्धि और दुर्गुण ही उत्पन्न करता है। सन्तान पर यह भार लदेगा तो उसका अपकार ही होगा।
पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाया जाना चाहिये, पर उस कीचड़ में इतनी गहराई तक नहीं फँसना चाहिये कि उबर सकना सम्भव न हो सके। मोह को भव बन्धनों में से प्रमुख माना गया है। उसी संकीर्ण दायरे में जकड़े हुए लोग, लोकमंगल का कर्तव्य पालन कर ही नहीं पाते। जिन्हें सभी के प्रति पारिवारिकता का भाव अपनाने का अवसर मिलता है, उनके लिये हर किसी को आत्मा मानने का, सभी की सेवा- सहायता करने का आनन्द मिलता है।
अहंकार मोटे अर्थों में घमण्ड समझा जाता है। अकड़ना, उद्धत- अशिष्ट व्यवहार करना, क्रोधग्रस्त रहना अहंकार की निशानी है। पर वस्तुत: वह और भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। फैशन, सजधज, श्रृंगार, ठाठ- बाट अपव्यय, सस्ता बड़प्पन आदि अहंकार परिवार के ही सदस्य हैं। लोग शेखीखोरी के लिये ढेरों समय, श्रम और पैसा खर्च करते देखे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है, जिसमें अपने को भले ही मजा आता हो, पर हर विचारशील को इसमें क्षुद्रता की, बचकानेपन की ही गन्ध आती है। इस विडम्बना के लिये चित्र- विचित्र प्रवंचनायें रचनी पड़ती हैं। ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करने में भी अहंता की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कलह और विग्रह प्राय: उसी कारण उत्पन्न होते हैं। आदमी की विशिष्टता अपनी विनयशीलता एवं दूसरों के सम्मान में निहित है। उसी कसौटी पर किसी की सज्जनता परखी जाती है। अहंकारी से उन सद्गुणों में से एक भी नहीं निभ पाता। अहंभाव को आत्मघाती शत्रु माना गया है। ऐसे लोगों से आत्मसाधना तो बन ही नहीं पाती। उन पर उद्दण्डता व दूसरों को नीचा दिखाने का भूत सदैव चढ़ा रहता है और दूसरों को गिराने एवं नीचा दिखाने की ही ललक उठती रहती है। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने में ही लगे रहते हैं। इन परिस्थितियों में आत्मोत्कर्ष और आत्मपरिष्कार कैसे बन पड़े?
लोभ, मोह और अहंकार के तीन भारी पत्थर जिन्होंने सिर पर लाद रखे हैं, उनके लिये जीवन साधना की लम्बी और ऊँची मंजिल पर चल सकना, चल पड़ना असम्भव हो जाता है। भले ही कोई कितना पूजा- पाठ क्यों न करता रहे! जिन्हें तथ्यान्वेषी बनना है, उन्हें इन तीन शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाना ही चाहिये।
हलकी वस्तुएँ पानी पर तैरती हैं, किन्तु भारी होने पर वे डूब जाती हैं। जो लोभ, मोह और अहंकार रूपी भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, उन्हें भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। जिन्हें तरना, तैरना है, उन्हें इन तीनों भारों को उतारने का प्रयत्न करना चाहिये।
अनेकानेक दोष- दुर्गुणों कषाय- कल्मषों का वर्गीकरण विभाजन करने पर उनकी संख्या हजारों हो सकती है, पर उनके मूल उद्गम यही तीन लोभ, मोह और अहंकार हैं। इन्हीं भव बन्धनों से मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जकड़े पड़े हैं। इनका उन्मूलन किये बिना आत्मा को उस स्वतन्त्रता का लाभ नहीं मिल सकता जिसे मोक्ष कहते हैं। इन तीनों पर कड़ी नजर रखी जाय। इन्हें अपना संयुक्त शत्रु माना जाये। इनसे पीछा छुड़ाने के लिये हर दिन नियमित रूप से प्रयास जारी रखा जाये। एकदम तो सब कुछ सही हो जाना कठिन है, पर उन्हें नित्यप्रति यथासम्भव घटाते- हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रखने पर सुधार क्रम में सफलता मिलती ही चलती है और एक दिन ऐसा भी आता है, जब इनसे पूरी तरह छुटकारा पाकर बन्धन मुक्त हुआ जा सके।
देखा यह जाता है कि भक्त भगवान् को साधता है। उसको मूर्ख समझते हुए उसकी गलतियाँ निकालता है। तरह- तरह के उलाहने देता है। साथ ही गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़कर, खींसें निपोरकर अपना- अपना अनुचित उल्लू सीधा करने के लिये जाल- जंजाल बुनता है। प्रशंसा के पुल बाँधता है। छिटपुट भेंट चढ़ाकर उसे फुसलाने का प्रयत्न करता है। समझा जाता है कि सामान्य लोगों से व्यावहारिक जगत में आदान- प्रदान के आधार पर ही लेन- देन चलता है, पर ईश्वर या देवता ऐसे हैं जिन्हें वाणी की वाचालता तथा शारीरिक- मानसिक उचक- मचक करने भर से वशवर्ती नहीं किया जा सकता है। यह दार्शनिक भूल मनुष्य को एक प्रकार से छिपा हुआ नास्तिक बना देती है। प्रकट नास्तिक वे हैं जो प्रत्यक्षवाद के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर न होने पर उसकी मान्यता से इंकार कर देते हैं। दूसरे छिपे नास्तिक वे हैं जो उससे पक्षपात की, मुफ्त में लम्बी- चौड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते रहते हैं। मनुष्य विधि व्यवस्था को तोड़ता- छोड़ता रहता है, पर ईश्वर के लिये यह सम्भव नहीं कि अपनी बनाई कर्मफल व्यवस्था का उल्लंघन करे या दूसरों को ऐसा करने के लिये उत्साहित करे। तथाकथित भक्त लोग ऐसी ही आशाएँ किया करते हैं। अन्ततः: उन्हें निराश ही होना पड़ता है। इस निराशा की खीज और थकान से वे या तो साधना- विधान को मिथ्या बताते हैं या ईश्वर के निष्ठुर होने की मान्यता बनाते हैं। कई पाखण्डी कुछ भी हस्तगत न होने पर भी प्रवंचना रचते हैं और नकटा सम्प्रदाय की तरह अपनी सिद्धि- सफलता का बखान करते हैं। आज का आस्तिकवाद इसी विडम्बना में फँसा हुआ है और वह लगभग नास्तिकवाद के स्तर पर जा पहुँचा है।
आवश्यकता हैं भ्रान्तियों से निकलने और यथार्थता को अपनाने की। इस दिशा में मान्यताओं को अग्रगामी बनाते हुए हमें सोचना होगा कि जीवन साधना ही आध्यात्मिक स्वस्थता और बलिष्ठता है। इसी के बदले प्रत्यक्ष जीवन में मरण की प्रतीक्षा किये बिना, स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि का रसास्वाद करते रहा जा सकता है। उन लाभों को हस्तगत किया जा सकता है, जिनका उल्लेख अध्यात्म विधा की महत्ता बताते हुए शास्त्रकारों ने विस्तारपूर्वक किया है। सच्चे सन्तों- भक्तों का इतिहास भी विद्यमान है। खोजने पर प्रतीत होता है कि पूजा- पाठ भले ही उनका न्यूनाधिक रहा है, पर उन्होंने जीवन साधना के क्षेत्र में परिपूर्ण जागरूकता बरती। इसमें व्यक्तिक्रम नहीं आने दिया। न आदर्श की अवज्ञा की और न उपेक्षा बरती। भाव- संवेदनाओं में श्रद्धा, विचार बुद्धि में प्रज्ञा और लोक व्यवहार में शालीन सद्भावना की निष्ठा अपनाकर कोई भी सच्चे अर्थों में जीवन देवता का सच्चा साधक बन सकता है। उसका उपहार, वरदान भी उसे हाथों हाथ मिलता चला जाता है।
ऋषियों, मनीषियों, सन्त- सुधारकों और वातावरण में ऊर्जा उभार देने वाले महामानवों की अनेकानेक साक्षियाँ विश्व इतिहास में भरी पड़ी हैं। इनमें से प्रत्येक को हर कसौटी पर जाँच- परखकर देखा जा सकता है कि उनमें से हर एक को अपना व्यक्तित्व उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ा है। इससे कम में किसी को भी न आत्मा की प्राप्ति हो सकी न परमात्मा की, न ऐसों का लोक बना, और न परलोक। पूजा को श्रृंगार माना जाता रहा है। स्वास्थ्य वास्तविक सुन्दरता है। ऊपर से स्वस्थ व्यक्ति को वस्त्राभूषणों से, प्रसाधन सामग्री से सजाया भी जा सकता है। इसे सोने में सुगन्ध का संयोग बन पड़ा माना जा सकता है। जीवन साधना समग्र स्वास्थ्य बनाने जैसी विधा है। उसके ऊपर पूजा- पाठ का श्रृंगार सजाया जाय तो शोभा और भी अधिक बढ़ेगी। इसमें सुरुचि तो है किन्तु यह नहीं माना जाना चाहिये कि मात्र श्रृंगार साधनों के सहारे किसी जीर्ण- जर्जर रुग्ण या मृत शरीर को सुन्दर बना दिया जाय तो प्रयोजन सध सकता है। इससे तो उलटा उपहास ही बढ़ता है। इसके विपरीत यदि कोई हृष्ट- पुष्ट पहलवान मात्र लँगोट पहनकर अखाड़े में उतरता है तो भी उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जीवन को सुसंस्कृत बना लेने वाले यदि पूजा- अर्चना के लिये कम समय निकाल पाते हैं तो भी काम चल जाता है।
अध्यात्म विज्ञान के साधकों को अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें सोचना होता है कि मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर का इस प्रकार उपयोग करना है, जिससे शरीर का निर्वाह लोक व्यवहार भी चलता रहे, पर साथ ही आत्मिक अपूर्णता को पूरी करने का चरम लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। ईश्वर के दरबार में पहुँचकर सीना तानकर यह कहा जा सके कि जो अमानत जिस प्रयोजन के लिये सौंपी गई थी, उसे उसी हेतु सही रूप में प्रयुक्त किया गया।
इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें तीन हैं। इन्हीं को रावण, कुम्भकरण, मेघनाथ कहा गया है। यह दैवी भागवत् के महिषासुर, मधुकैटभ, रक्तबीज हैं। ये प्राय: साथ लगे रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं के कारण मनुष्य पतन और पराभव के गर्त में जा गिरता है। पशु, प्रेत और पिशाच की जिन्दगी जीता है। नर- वानर और नर- पामर के रूप में इन्हीं के चंगुल में फँसे हुए लोगों को देखा जाता है। ये तीन हैं- लोभ मोह एवं अहंकार। वासना, तृष्णा और कुत्सा इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है।
लोक विजय के लिये सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धान्त अपनाना पड़ता है। औसत नागरिक स्तर के निर्वाह में सन्तोष करना पड़ता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। लालची के लिये अनीति अपनाये बिना तृष्णा की पूर्ति कर सकना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं होता। जो व्यक्ति विलास में अधिक खर्च करता है, वह प्रकारान्तर से दूसरों को उतना ही अभावग्रस्त रहने के लिये मजबूर करता है। इसीलिये शास्त्रकारों ने परिग्रह को पाप बताया है। विलासी, संग्रही, अपव्ययी की भी ऐसी निन्दा की गई है।
अधिक कमाया जा सकता है, पर उसमें से निजी निर्वाह में सीमित व्यय करके शेष बचत क गिरों को उठाने, उठों को उछालने और सत्प्रवृत्तियों के संवर्द्धन में लगाया जाना चाहिये। राजा जनक जैसे उदाहरणों की कमी नहीं। मितव्ययी अनेक दुर्व्यसनों और अनाचारों से बचता है। ऐसी हविश उसे सताती नहीं जिसके लिये अनाचार पर उतारू होना पड़े। साधु- ब्राह्मणों की यही परम्परा रही है। सज्जनों की शालीनता भी उसी आधार पर फलती- फूलती रही है। जीवन साधना के उस प्रथम अवरोध ‘लोभ’ को नियन्त्रित कराने वाला दृष्टिकोण हर जीवन साधना के साधक को अपनाना ही चाहिये।
मोह वस्तुओं से भी होता है और व्यक्तियों से भी। छोटे दायरे में आत्मीयता सीमाबद्ध करना ही मोह है। उसके रहते हृदय की विशालता चरितार्थ ही नहीं होती। अपना शरीर और परिवार ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। उन्हीं के लिये मरने- खपने के कुचक्र में फँसे रहना पड़ता है। ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के दो आत्मवादी सिद्धान्त हैं। इनमें से एक को भी ‘मोहग्रस्त’ कार्यान्वित नहीं कर सकता। इसलिये अपने में सबको और सबमें अपने को देखने की दृष्टि विकसित करना जीवन साधना के लिये आवश्यक माना गया है।
परिवार छोटे से छोटा रखा जाय। पूर्ववर्ती अभिभावकों, बड़ों और आश्रितों के ऋणों को चुकाने की ही व्यवस्था नहीं बन पाती तो नये अतिथियों को क्यों न्यौत बुलाया जाय? समय की विषमता को देखते हुए अनावश्यक बच्चे उत्पन्न कर परिवार का भार बढ़ाना परले सिरे की भूल है। समान विचारों का साथी- सहयोगी मिले तो विवाह करने में हर्ज नहीं, पर वह एक दूसरे की सहायता सेवा करते हुए प्रगतिपथ पर अग्रसर होने के लिये ही किया जाना चाहिये। जिन्हें सन्तान की बहुत ललक हो, वे निर्धनों के बच्चे पालने के लिये ले सकते हैं। परिवार को स्वावलम्बी और सुसंस्कारी बनाना पर्याप्त है। औलाद के लिये विपुल सम्पदा उत्तराधिकार में छोड़ मरने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिये। मुफ्त का माल किसी को भी हजम नहीं होता। वह दुर्बुद्धि और दुर्गुण ही उत्पन्न करता है। सन्तान पर यह भार लदेगा तो उसका अपकार ही होगा।
पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाया जाना चाहिये, पर उस कीचड़ में इतनी गहराई तक नहीं फँसना चाहिये कि उबर सकना सम्भव न हो सके। मोह को भव बन्धनों में से प्रमुख माना गया है। उसी संकीर्ण दायरे में जकड़े हुए लोग, लोकमंगल का कर्तव्य पालन कर ही नहीं पाते। जिन्हें सभी के प्रति पारिवारिकता का भाव अपनाने का अवसर मिलता है, उनके लिये हर किसी को आत्मा मानने का, सभी की सेवा- सहायता करने का आनन्द मिलता है।
अहंकार मोटे अर्थों में घमण्ड समझा जाता है। अकड़ना, उद्धत- अशिष्ट व्यवहार करना, क्रोधग्रस्त रहना अहंकार की निशानी है। पर वस्तुत: वह और भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। फैशन, सजधज, श्रृंगार, ठाठ- बाट अपव्यय, सस्ता बड़प्पन आदि अहंकार परिवार के ही सदस्य हैं। लोग शेखीखोरी के लिये ढेरों समय, श्रम और पैसा खर्च करते देखे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है, जिसमें अपने को भले ही मजा आता हो, पर हर विचारशील को इसमें क्षुद्रता की, बचकानेपन की ही गन्ध आती है। इस विडम्बना के लिये चित्र- विचित्र प्रवंचनायें रचनी पड़ती हैं। ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करने में भी अहंता की ही प्रमुख भूमिका रहती है। कलह और विग्रह प्राय: उसी कारण उत्पन्न होते हैं। आदमी की विशिष्टता अपनी विनयशीलता एवं दूसरों के सम्मान में निहित है। उसी कसौटी पर किसी की सज्जनता परखी जाती है। अहंकारी से उन सद्गुणों में से एक भी नहीं निभ पाता। अहंभाव को आत्मघाती शत्रु माना गया है। ऐसे लोगों से आत्मसाधना तो बन ही नहीं पाती। उन पर उद्दण्डता व दूसरों को नीचा दिखाने का भूत सदैव चढ़ा रहता है और दूसरों को गिराने एवं नीचा दिखाने की ही ललक उठती रहती है। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करने में ही लगे रहते हैं। इन परिस्थितियों में आत्मोत्कर्ष और आत्मपरिष्कार कैसे बन पड़े?
लोभ, मोह और अहंकार के तीन भारी पत्थर जिन्होंने सिर पर लाद रखे हैं, उनके लिये जीवन साधना की लम्बी और ऊँची मंजिल पर चल सकना, चल पड़ना असम्भव हो जाता है। भले ही कोई कितना पूजा- पाठ क्यों न करता रहे! जिन्हें तथ्यान्वेषी बनना है, उन्हें इन तीन शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाना ही चाहिये।
हलकी वस्तुएँ पानी पर तैरती हैं, किन्तु भारी होने पर वे डूब जाती हैं। जो लोभ, मोह और अहंकार रूपी भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादे हुए हैं, उन्हें भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। जिन्हें तरना, तैरना है, उन्हें इन तीनों भारों को उतारने का प्रयत्न करना चाहिये।
अनेकानेक दोष- दुर्गुणों कषाय- कल्मषों का वर्गीकरण विभाजन करने पर उनकी संख्या हजारों हो सकती है, पर उनके मूल उद्गम यही तीन लोभ, मोह और अहंकार हैं। इन्हीं भव बन्धनों से मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जकड़े पड़े हैं। इनका उन्मूलन किये बिना आत्मा को उस स्वतन्त्रता का लाभ नहीं मिल सकता जिसे मोक्ष कहते हैं। इन तीनों पर कड़ी नजर रखी जाय। इन्हें अपना संयुक्त शत्रु माना जाये। इनसे पीछा छुड़ाने के लिये हर दिन नियमित रूप से प्रयास जारी रखा जाये। एकदम तो सब कुछ सही हो जाना कठिन है, पर उन्हें नित्यप्रति यथासम्भव घटाते- हटाते चलने की प्रक्रिया जारी रखने पर सुधार क्रम में सफलता मिलती ही चलती है और एक दिन ऐसा भी आता है, जब इनसे पूरी तरह छुटकारा पाकर बन्धन मुक्त हुआ जा सके।
Versions
-
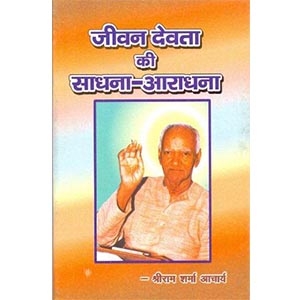
HINDIजीवन देवता की साधना आराधनाScan Book Version
-
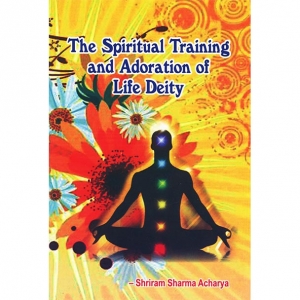
ENGLISHThe Spiritual Training and Adoration of Life DeityScan Book Version
-
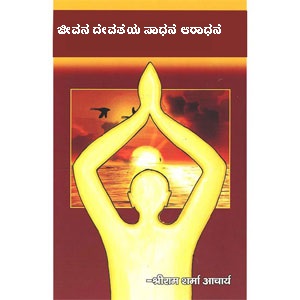
KANNADAಜೀವನ ದೇವತೆಯ ಸಾಧನೆ ಆರಾಧನೆScan Book Version
-
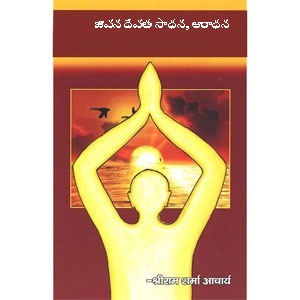
TELUGUజీవన దేవత సాధన, ఆరాధనScan Book Version
-
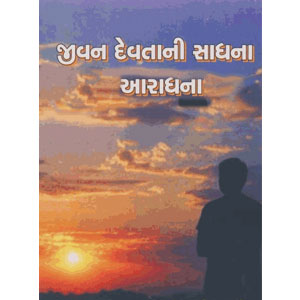
GUJRATIજીવન દેવતાની સધના-આરાધનાScan Book Version
-
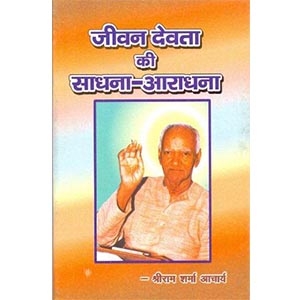
HINDIजीवन देवता की साधना-आराधनाText Book Version

