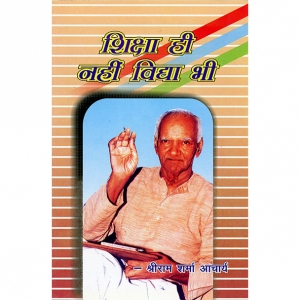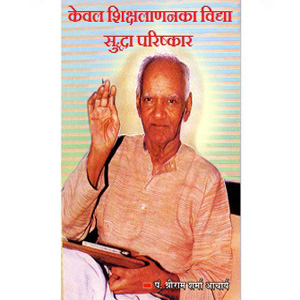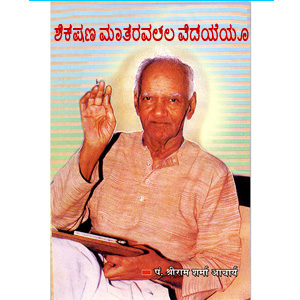शिक्षा ही नहीं विद्या भी 
तीर्थयात्रा का आदर्श
Read Scan Version
दक्षिण अफ्रीका से जब गाँधी जी भारत लौटे और उन्होंने देश सेवा में लगने की इच्छा व्यक्त की, तो गोखले जी ने उन्हें प्रथम परामर्श दिया कि पहले एक बार समूचे देश की यात्रा कर ले और यह जानें कि लोगों की परिस्थितियाँ क्या हैं। गाँधी जी सहमत हो गये । दौरे पर निकले और देश के पिछड़ेपन का दृश्य देखकर मन में एक कसक लेकर वापस लौटे। कुछ महिलाओं को आधी धोती पहन कर नहाते और दूसरा पल्ला सुखा कर पहनते देखा, तो वे उस गरीबी पर द्रवित हो उठे और उसी दिन से उनने आधी धोती पहनने और ओढ़ने का व्रत लिया।
खुशहाली के वातावरण में रहने और चैन की जिंदगी बिताने वालों को यह पता ही नहीं कि देशवासी किस स्थिति में रह रहे हैं और पड़ोसियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का क्या अर्थ होता है? यह जानकारी देशाटन से ही प्रत्यक्ष अनुभव में आती है ।
‘‘पिकनिक’’ मन हल्का करने का एक अच्छा मनोरंजन माना जाता है। सभ्य समुदाय के लोग इसे अत्यन्त प्रभावशाली और सार्थक विनोद मानते हैं। पर्यटन के लिए सरकारी महकमें भी अपने कर्मचारियों को, विद्यार्थियों-अध्यापकों को छुट्टी देते हैं; ताकि वे नई ताजगी लेकर वापस लौट सकें और भविष्य में अधिक उत्साहपूर्वक काम कर सकें।
पुरातन काल में उस प्रक्रिया के साथ धार्मिकता भी जोड़ दी जाती थी। जो जत्थे प्रवास पर निकलते, वे रास्ते में नारे लगाते, गीत गाते और दीवालों पर आदर्श वाक्य लिखते जाते थे। जहाँ ठहरने का निर्धारण होता था, वहाँ पूर्व सूचना भिजवा दी जाती थी ताकि स्थानीय लोग एकत्रित होकर तीर्थ यात्रियों में से जो वक्ता, गायक धर्म सेवी होते थे, उनके प्रवचन सुनकर अपनी जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन, सुधार कर सकें।
तीर्थ यात्राएँ वाहनों से नहीं होती थीं, उनके लिए पैदल ही चलना पड़ता था। अभी भी ब्रज-चौरासी कोस, प्रयाग की पाँच-कोसी परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा आदि के लिए पैदल ही निकलते हैं, ताकि यात्री अनुभव संपादन, पारस्परिक परिचय एवं स्वास्थ्य संवर्धन की त्रिविध प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें । अब पैदल चलने और कंधे पर आवश्यक सामान लादकर चलने का प्रचलन नहीं रहा, तो साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। वह भी पैरों की शक्ति से चलती है, पर समय बचत करती है, जन संपर्क भी संभव बनाती है।
इन दिनों लोग रेल-मोटरों में दौड़ लगाते, किसी देवता की प्रतिमा का दर्शन करते और जलाशयों में डुबकी लगाकर वापस लौट आते हैं। बड़े मंदिर देखने का विशेष आकर्षण रहता है, जो प्राय: बड़े नगरों में ही विनिर्मित होते हैं, जबकि असली भारत देहातों में रहता है। वहीं की समस्याएँ देश की समस्याएँ है। वहीं की प्रगति से देश के प्रगतिशील होने की आशा की जाती है। इसलिए तीर्थ यात्राएँ पैदल की जाती थीं। कम समय खाली होने पर तीर्थयात्री अपने आस-पास का ही प्रवास क्रम बना लेते थे। उसी मार्ग में आने वाले छोटे-बड़े देवालयों, नदी, सरोवरों पुरातन वृक्षों, उद्यानों का दर्शन करके अपनी धर्म जिज्ञासा पूरी करते थे।
जिनके पास अधिक समय होता था, वे मँझोले तीर्थों में चलते रहने वाले धर्म-सम्मेलनों में योजनाबद्ध प्रशिक्षण और साथ ही जुड़े हुए साधना क्रम को भी संपन्न कर लेते थे। छोटे-बड़ेे देवालय प्राय: हर गाँव में होते थे। उनमें इतनी जगह भी सुरक्षित रहती थी कि तीर्थ यात्रियों की कई टोलियाँ आए, तो वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सकें; स्थानीय लोग उन तक पहुँचकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकें।
देवालयों में दान-दक्षिणा एवं अन्न श्रद्धालु लोग पहुँचाते रहते थे। उससे स्थानीय कार्यकर्ता, पुजारी का निर्वाह तो चल ही जाता था, तीर्थ यात्रियों को भी बनाने-खाने की कच्ची सामग्री मिल जाती थी। इस आधार पर छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों को तीर्थ-यात्रियों द्वारा दी गई प्रेरणाओं का लाभ मिलता रहता था।
बड़े मंदिर प्राय: बड़े शहरों में ही बने हुए हैं। वहाँ रेल, मोटरों से दौड़े जाने, घिच-पिच बढ़ाने, धक्के खाने से किस प्रकार धर्म-लाभ मिल सकता है, यह समझ से बाहर की बात है। जिसके साथ धर्म-प्रचार जुड़ा हुआ न हो, उसके द्वारा किसे, किस प्रकार धर्म लाभ मिलेगा? जहाँ क्रमबद्ध साधनाएँ, शिक्षण, सत्संग की व्यवस्था न हो, उन देवालय क्षेत्रों में क्या किसी को कुछ लाभ मिलेगा?
गंगाजल की काँवर कंधे पर रखकर अपने निकटवर्ती शिवालय पर चढ़ाने और रास्ते को पैदल पार करते हुए मार्ग में प्रेरक भजन गाते चलने का रिवाज अभी भी बहुत जगह है। इस आधार पर पुरातन परंपरा के पीछे सन्निहित उद्देश्यों का तो स्मरण आता ही है। यह क्रम प्रतिमाएँ झाँकते फिरने, डुबकी लगाते फिरने और पात्र-कुपात्रों से जेब कटाते फिरने की अपेक्षा कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण है।
शान्तिकुञ्ज को तीर्थ केन्द्र मानकर विभिन्न शाखा केन्द्रों से साइकिल टोलियाँ चलती रहती हैं। रास्ते की दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखते, मिल-जुलकर गीत गाते, लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते, विश्राम स्थलों पर सत्संग सम्पन्न करती हुई, वहाँ पहुँचती रहती हैं। जिनसे दूर की यात्रा नहीं बन पड़ती, वे अपने समीप ही प्राय: एक सप्ताह का कार्यक्रम बना लेते हैं और उस परिधि में नव युग के अनुरूप नव जीवन का संचार करते हैं।
अचल तीर्थ वे हैं, जो ईंट, चूने, सीमेंट जैसे जड़ पदार्थों से बने होते हैं; अपनी जगह स्थिर रहते हैं। लोगों को उनके दर्श-स्पर्श के लिए जाना पड़ता है। उनकी महिमा-गरिमा तो है, पर उनसे अधिक नहीं, जो जीवंत होते, चलते-फिरते और प्राण-चेतना बिखेरने गली-मुहल्लों में घर-द्वारों पर बिना बुलाए ही जा पहुँचते हैं। किसी जमाने में साधु ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक इसी प्रयोजन को लेकर निरंतर भ्रमण करते रहते थे और जन-जीवन में आदर्शों की प्रतिष्ठापना का शंख बजाते थे। अब लगता है उसका प्रचलन उठ गया। जड़ता ने अब अहंकार में, आलस्य-प्रमाद के रूप में ऐसी रीति-नीति अपना ली है, जिसमें घर बैठे ही प्रचुर मात्रा में सम्मान, सुविधा और साधन उपलब्ध होते रहें। प्रतीत होता है कि अचल देवालयों की तुलना में जिन चल देवालयों का पुण्य-प्रताप असंख्य गुना माना जाता है, उसका कलियुगी प्रभाव से अस्तित्व ही उठ गया।
इसे फिर से जीवित-जाग्रत करने की आवश्यकता है, अन्यथा जिनमें लंबी दूरी पार करने और पैसा खर्चने की सामर्थ्य नहीं है, वे तीर्थों की धर्म-धारणा से वंचित ही रह जाएँगे।
पिछले लेखों में बताया जा चुका है कि वक्ताओं, गायकों के स्तर वाले परिव्राजकों का अभाव देखते हुए समय की माँग पूरी करने के लिए शान्तिकुञ्ज ने कुछ नए उपकरण इन्हीं दिनों बनाए हैं, जो उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इनके सहारे कोई भी शिक्षित-अशिक्षित अपने आप को चल तीर्थ बना सकता है और हाट-बाजारों में गली-कूचों में, पार्कों-सड़कों भीड़ भरे क्षेत्रों में अलख जगाते रहने का निरंतर कार्य कर सकता है। साधु-ब्राह्मणों का लगभग अभाव हो जाने की स्थिति में नैष्ठिक साधकों द्वारा, इन यंत्रों के सहारे भी सचल-सार्थक तीर्थ यात्राओं की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।
खुशहाली के वातावरण में रहने और चैन की जिंदगी बिताने वालों को यह पता ही नहीं कि देशवासी किस स्थिति में रह रहे हैं और पड़ोसियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का क्या अर्थ होता है? यह जानकारी देशाटन से ही प्रत्यक्ष अनुभव में आती है ।
‘‘पिकनिक’’ मन हल्का करने का एक अच्छा मनोरंजन माना जाता है। सभ्य समुदाय के लोग इसे अत्यन्त प्रभावशाली और सार्थक विनोद मानते हैं। पर्यटन के लिए सरकारी महकमें भी अपने कर्मचारियों को, विद्यार्थियों-अध्यापकों को छुट्टी देते हैं; ताकि वे नई ताजगी लेकर वापस लौट सकें और भविष्य में अधिक उत्साहपूर्वक काम कर सकें।
पुरातन काल में उस प्रक्रिया के साथ धार्मिकता भी जोड़ दी जाती थी। जो जत्थे प्रवास पर निकलते, वे रास्ते में नारे लगाते, गीत गाते और दीवालों पर आदर्श वाक्य लिखते जाते थे। जहाँ ठहरने का निर्धारण होता था, वहाँ पूर्व सूचना भिजवा दी जाती थी ताकि स्थानीय लोग एकत्रित होकर तीर्थ यात्रियों में से जो वक्ता, गायक धर्म सेवी होते थे, उनके प्रवचन सुनकर अपनी जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन, सुधार कर सकें।
तीर्थ यात्राएँ वाहनों से नहीं होती थीं, उनके लिए पैदल ही चलना पड़ता था। अभी भी ब्रज-चौरासी कोस, प्रयाग की पाँच-कोसी परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा आदि के लिए पैदल ही निकलते हैं, ताकि यात्री अनुभव संपादन, पारस्परिक परिचय एवं स्वास्थ्य संवर्धन की त्रिविध प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें । अब पैदल चलने और कंधे पर आवश्यक सामान लादकर चलने का प्रचलन नहीं रहा, तो साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। वह भी पैरों की शक्ति से चलती है, पर समय बचत करती है, जन संपर्क भी संभव बनाती है।
इन दिनों लोग रेल-मोटरों में दौड़ लगाते, किसी देवता की प्रतिमा का दर्शन करते और जलाशयों में डुबकी लगाकर वापस लौट आते हैं। बड़े मंदिर देखने का विशेष आकर्षण रहता है, जो प्राय: बड़े नगरों में ही विनिर्मित होते हैं, जबकि असली भारत देहातों में रहता है। वहीं की समस्याएँ देश की समस्याएँ है। वहीं की प्रगति से देश के प्रगतिशील होने की आशा की जाती है। इसलिए तीर्थ यात्राएँ पैदल की जाती थीं। कम समय खाली होने पर तीर्थयात्री अपने आस-पास का ही प्रवास क्रम बना लेते थे। उसी मार्ग में आने वाले छोटे-बड़े देवालयों, नदी, सरोवरों पुरातन वृक्षों, उद्यानों का दर्शन करके अपनी धर्म जिज्ञासा पूरी करते थे।
जिनके पास अधिक समय होता था, वे मँझोले तीर्थों में चलते रहने वाले धर्म-सम्मेलनों में योजनाबद्ध प्रशिक्षण और साथ ही जुड़े हुए साधना क्रम को भी संपन्न कर लेते थे। छोटे-बड़ेे देवालय प्राय: हर गाँव में होते थे। उनमें इतनी जगह भी सुरक्षित रहती थी कि तीर्थ यात्रियों की कई टोलियाँ आए, तो वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सकें; स्थानीय लोग उन तक पहुँचकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकें।
देवालयों में दान-दक्षिणा एवं अन्न श्रद्धालु लोग पहुँचाते रहते थे। उससे स्थानीय कार्यकर्ता, पुजारी का निर्वाह तो चल ही जाता था, तीर्थ यात्रियों को भी बनाने-खाने की कच्ची सामग्री मिल जाती थी। इस आधार पर छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों को तीर्थ-यात्रियों द्वारा दी गई प्रेरणाओं का लाभ मिलता रहता था।
बड़े मंदिर प्राय: बड़े शहरों में ही बने हुए हैं। वहाँ रेल, मोटरों से दौड़े जाने, घिच-पिच बढ़ाने, धक्के खाने से किस प्रकार धर्म-लाभ मिल सकता है, यह समझ से बाहर की बात है। जिसके साथ धर्म-प्रचार जुड़ा हुआ न हो, उसके द्वारा किसे, किस प्रकार धर्म लाभ मिलेगा? जहाँ क्रमबद्ध साधनाएँ, शिक्षण, सत्संग की व्यवस्था न हो, उन देवालय क्षेत्रों में क्या किसी को कुछ लाभ मिलेगा?
गंगाजल की काँवर कंधे पर रखकर अपने निकटवर्ती शिवालय पर चढ़ाने और रास्ते को पैदल पार करते हुए मार्ग में प्रेरक भजन गाते चलने का रिवाज अभी भी बहुत जगह है। इस आधार पर पुरातन परंपरा के पीछे सन्निहित उद्देश्यों का तो स्मरण आता ही है। यह क्रम प्रतिमाएँ झाँकते फिरने, डुबकी लगाते फिरने और पात्र-कुपात्रों से जेब कटाते फिरने की अपेक्षा कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण है।
शान्तिकुञ्ज को तीर्थ केन्द्र मानकर विभिन्न शाखा केन्द्रों से साइकिल टोलियाँ चलती रहती हैं। रास्ते की दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखते, मिल-जुलकर गीत गाते, लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते, विश्राम स्थलों पर सत्संग सम्पन्न करती हुई, वहाँ पहुँचती रहती हैं। जिनसे दूर की यात्रा नहीं बन पड़ती, वे अपने समीप ही प्राय: एक सप्ताह का कार्यक्रम बना लेते हैं और उस परिधि में नव युग के अनुरूप नव जीवन का संचार करते हैं।
अचल तीर्थ वे हैं, जो ईंट, चूने, सीमेंट जैसे जड़ पदार्थों से बने होते हैं; अपनी जगह स्थिर रहते हैं। लोगों को उनके दर्श-स्पर्श के लिए जाना पड़ता है। उनकी महिमा-गरिमा तो है, पर उनसे अधिक नहीं, जो जीवंत होते, चलते-फिरते और प्राण-चेतना बिखेरने गली-मुहल्लों में घर-द्वारों पर बिना बुलाए ही जा पहुँचते हैं। किसी जमाने में साधु ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक इसी प्रयोजन को लेकर निरंतर भ्रमण करते रहते थे और जन-जीवन में आदर्शों की प्रतिष्ठापना का शंख बजाते थे। अब लगता है उसका प्रचलन उठ गया। जड़ता ने अब अहंकार में, आलस्य-प्रमाद के रूप में ऐसी रीति-नीति अपना ली है, जिसमें घर बैठे ही प्रचुर मात्रा में सम्मान, सुविधा और साधन उपलब्ध होते रहें। प्रतीत होता है कि अचल देवालयों की तुलना में जिन चल देवालयों का पुण्य-प्रताप असंख्य गुना माना जाता है, उसका कलियुगी प्रभाव से अस्तित्व ही उठ गया।
इसे फिर से जीवित-जाग्रत करने की आवश्यकता है, अन्यथा जिनमें लंबी दूरी पार करने और पैसा खर्चने की सामर्थ्य नहीं है, वे तीर्थों की धर्म-धारणा से वंचित ही रह जाएँगे।
पिछले लेखों में बताया जा चुका है कि वक्ताओं, गायकों के स्तर वाले परिव्राजकों का अभाव देखते हुए समय की माँग पूरी करने के लिए शान्तिकुञ्ज ने कुछ नए उपकरण इन्हीं दिनों बनाए हैं, जो उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इनके सहारे कोई भी शिक्षित-अशिक्षित अपने आप को चल तीर्थ बना सकता है और हाट-बाजारों में गली-कूचों में, पार्कों-सड़कों भीड़ भरे क्षेत्रों में अलख जगाते रहने का निरंतर कार्य कर सकता है। साधु-ब्राह्मणों का लगभग अभाव हो जाने की स्थिति में नैष्ठिक साधकों द्वारा, इन यंत्रों के सहारे भी सचल-सार्थक तीर्थ यात्राओं की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।