लोकसेवियों के लिए दिशाबोध 
सेवा धर्म के मार्ग में बाधाएँ और भटकाव
Read Scan Version
सेवा का महत्त्व और जीवन विकास के लिए उसकी आवश्यकता समझ लेने के बाद सेवा धर्म की उमंग उठना स्वाभाविक है। अधिकांश लोगों में इस तरह की उमंग उठती है। वे उस उमंग के अनुरूप सेवा के मार्ग में प्रवृत्त भी होते हैं, किन्तु उस पथ पर अधिक समय तक नहीं चल पाते। इसका कारण यह है कि लोकसेवा के प्रति आवश्यक उत्साह और निष्ठा का जागरण नहीं हो पाया। कुछ लोग प्रवृत्त भी होते हैं, पर कठिनाइयाँ आती देख कर, उसे झमेला समझ कर छोड़ बैठते हैं अथवा असफलता से डर कर चुप बैठ जाते हैं ।
बहुत से कारण हैं जिनमें सेवा कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाती। लोग या तो गलत बातों को सही समझ कर विचलित हो जाते हैं अथवा सफलता का अहंकार उन्हें दिग्भ्रांत कर देता है। इन सब बाधाओं और भटकाव की परिस्थितियों को पहले से जान समझकर चला जाए, तो सेवाधर्म का निर्वाह, पालन किया जा सकता है। होता यह भी है कि सेवा धर्म अपना लेने के बाद उसे अपना जीवन लक्ष्य बनाने तथा उसे साधना स्तर पर करने में भूल हो जाती है। भूलें स्वभावगत हों या परिस्थितियों के कारण, लोक सेवी को उसके साधना पथ से दूर हटाती हैं ।
हमें यह तथ्य स्मरण रखना चाहिये कि मार्गदर्शक बनना हो, तो नेतृत्त्व का कौशल नहीं चरित्र चाहिए। प्राचीनकाल में लोकमानस के परिष्कार का महान् कार्य जो लोग हाथ में लेते थे, वे कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व ब्राह्मणों जैसी संयमशीलता और साधु जैसी उदार आत्मीयता का अभ्यास करते थे। इस परीक्षा में वे जितनी ऊँची कक्षा उत्तीर्ण करते थे, उसी अनुपात से उनकी सेवा- साधना सफल होती थी । यदि सच्चे मन से उच्चस्तरीय दृष्टिकोण लेकर सेवाधर्म अपनाया जाय, तो उसका परिणाम लोक- मंगल से भी अधिक आत्मोत्कर्ष के रूप में उपलब्ध होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा परिजनों को युगशिल्पी की भूमिका निभाने के लिए अग्रसर होते समय इस बात को गिरह बाँधकर रखना है कि उन्हें अपने स्तर से, व्यक्तित्व की दृष्टि से सामान्य लोगों की तुलना में कहीं ऊँचा उठकर रहना है ।
इसके लिए क्या करना होगा? इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर्तृत्व उतना नहीं है जितना कि दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रबल अभ्यास अपनाना। सर्वविदित है कि लोभ- मोह के भव- बन्धन आदर्शवादिता के, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले के लिए हथकड़ी- बेड़ियाँ जैसे अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची, संग्रही, विलासी व्यक्ति को लाभ लिप्सा इस कदर जकड़े रहती है कि उसे परमार्थ में कोई रस ही नहीं आता। अपनी तराजू पर अपने बाटों से तौलने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हलका। इसलिए लालच में राई- रत्ती कमी पड़ते ही वह परमार्थ से हाथ खींच लेता है और कुछ आडम्बर करता भी है, तो उतना ही जिससे कम खर्च में लोकसेवी पुण्यात्मा की अधिक ख्याति खरीदी जा सके। इसमें भी वे तोलते रहते हैं कि कितना गँवाया और कितना कमाया ।
दूसरा अवरोध है- व्यामोह। शरीर और परिवार के साथ अत्यधिक ममता जोड़ने वाले उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उचित- अनुचित कुछ भी करते रहते हैं। उन्हें यह छोटी परिधि लोक- परलोक सभी से बढ़कर प्रतीत होती है और उसी के निमित्त कोल्हू की तरह पिसते, आग की तरह जलते और बर्फ की तरह पिघलते रहते हैं। परिवार का उत्तरदायित्व निभाना, परिजनों के प्रति कर्तव्यपालन करना एक बात है और उन्हें सुविधाओं से लाद- लाद कर अनुचित दुलार से व्यक्तित्व की दृष्टि से हेय हीन बना देना सर्वथा दूसरी। मोहग्रस्त लोग दूसरी को अपनाते हैं और पहली की ओर से आँखें बन्द किए रहते हैं। इसके लिए कभी रोका झिड़का जाय कि उन पर अशर्फियाँ लुटाते रहने की तुलना में कहीं अधिक हित इसमें है कि वे श्रेष्ठ चिन्तन देने का प्रयास करें, मात्र लाड़- दुलार न दें, तो यह बात कोई मोहान्ध सुनता नहीं। पर कहे कौन किससे? ज्ञान वैराग्य की कथा कहते रहने वाले ही जब श्रोता भक्तजनों से भी अधिक गए- गुजरे सिद्ध होते हों, तो ‘ सत्य वचन, महाराज ’ की विडम्बना ही सिर हिलाती रहेगी।
परिवार पोषण किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नयी दृष्टि से देखने से इस परिकर के कितने ही सदस्य ऐसे होते हैं, जिनमें आर्थिक स्वावलम्बन की ही नहीं, दूसरों को सहारा देने की भी क्षमता है, किन्तु उन्हें मोहवश अथवा नाक कटने के डर से अपंग अपाहिज बनाकर रखा गया है। एक कमाऊ व्यक्ति ही मरता- खपता रहता है, दूसरे समर्थ होते हुए भी असमर्थों की विरादरी में आलसी, प्रमादी बनें बैठे रहते हैं। इसी प्रकार फिजूल खर्ची की आदतें जब अभ्यास में आ जाती हैं तो खर्च का ढोल इतना भारी हो जाता है कि उसे भी परिपोषण की संज्ञा मिलती है, वस्तुतः यह होता परिवार पोषण भर है। पोषण सरल है, तोषण अति कठिन है। पुत्रवधू की गोद से छीन- छीन कर पोते- पोतियों को कंधे पर लादे फिरने वाले बुड्ढों की भी कमी नहीं। कमाऊ लड़कों के गुलछर्रे उड़ाने में कोई कमी न रहने पर भी बुड्ढा जब उन्हीं के हाथ में पेन्शन थमाता जाता है, तो उसकी ‘ दयालुता ’ देखते ही बनती है। जीवन भर की कमाई का बँटवारा जब समर्थ बेटों की हिस्सेदारी के रूप में कर दिया जाता है, तो प्रतीत होता है कि घिनौना व्यामोह किस प्रकार औचित्य एवं प्रचलन का लबादा ओढ़कर अपने को निर्दोष सिद्ध करता है ।
इस चक्रव्यूह के कुछ थोड़े से घेरे ही यहाँ उजागर किये हैं। ऐसे- ऐसे और भी अनेकों हैं, जिनमें आये दिन बच्चे जनने, उस पर खुशी मनाने और सिर पर पर्वतों जैसे बोझ बढ़ाते चलने की भी एक बात सम्मिलित की जा सकती है। इस मोह ग्रस्तता को परमार्थ पथ पर अड़ी हुई भारी चट्टान कह सकते हैं। लोभ को प्रथम नम्बर दिया जाता है मोह को दूसरा, पर अभी यह तय किया जाना है कि इनमें से कौन द्वितीय है, वस्तुतः यह रावण, अहिरावण जैसे सगे भाई प्रतीत होते हैं ।
आत्म- कल्याण और लोक- कल्याण की साधना में ऐसा कुछ नहीं, जिसके लिए शरीर निर्वाह एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने में कोई बाधा पड़ती हो। मात्र लोभ और मोह का मद्यपों जैसा अतिवाद ही एक मात्र अवरोध है जो वस्तुतः तिनके जैसा हलका होते हुए भी पर्वत जैसा भारी बनकर दिग्भ्रान्तों के मनःक्षेत्र पर भूत- पिशाच की तरह चढ़ बैठता है और भली- चंगी परिस्थिति होते हुए भी नारकीय उत्पीड़नों की तरह निरन्तर संत्रस्त करता रहता है । किन्तु बात इतनी छोटी है नहीं। इस मार्ग में एक और बड़ा अवरोध ‘ अहंता ’ का है। यह परोक्ष होती है। न अपनी पकड़ में आती है, न दूसरों की परख में। इसलिए उसकी उखाड़- पछाड़ भी नहीं होती। फलतः मजे में अपने कोंतर में बैठी पोषण पाती, जोंक की तरह मोटी होती रहती है। इसकी विनाश लीला इतनी बड़ी है जिसकी तुलना में लोभ- मोह से होने वाली हानि को नगण्य जितना ठहराया जा सकता है ।
अहंता बड़प्पन पाने की आकांक्षा को कहते हैं। दूसरों की तुलना में अपने को अधिक महत्त्व, गौरव, श्रेय, पद, सम्मान मिलना चाहिए। यही है अहंता की आकांक्षा। इस जादूगरनी द्वारा लोगों को चित्र- विचित्र विडम्बनाएँ रचते देखा जा सकता है। केश, वस्त्र, आभूषण, सौन्दर्य प्रसाधनों की इन दिनों धूम है। फैशन के नाम पर कितना धन और कितना समय नष्ट होता है, उसे शरीर सज्जा में रुचि रखने वाले सभी जानते हैं। उस महँगे जंजाल को इसलिए रचना पड़ता है कि अहंता अपने को सुन्दर, युवा, आकर्षक, सभ्य, अमीर, सिद्ध करने के लिए इस लबादे को ओढ़कर वस्तुस्थिति से भिन्न प्रकार का प्रदर्शन करने को बाधित करती है। इसके बाद ठाट- बाट का नम्बर आता है। इसमें अमीरी का प्रदर्शन है। निवास, फर्नीचर, वाहन, नौकर तथा विलासिता के उपकरणों का सरंजाम जुटाने तथा रख- रखाव में इतना धन तथा मनोयोग लगता है, जो वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अनेक गुना मँहगा होता है। बात- बात में फिजूलखर्ची उस समय की जाती है जब उसे लोग देखें और अनुमान लगायें कि यह व्यक्ति धन कुबेर है और अनावश्यक खर्चने से भी इसे कोई कमी नहीं पड़ती। बड़प्पन पाने की मृगतृष्णा में लोग कितने पाखण्ड रचते, धन को पानी की तरह बहाने के उपरान्त आवश्यक प्रयोजनों में किस प्रकार कटौती करते हैं- इसे देखकर कोई सूक्ष्मदर्शी आश्चर्यचकित ही रह सकता है। असलियत का अनुमान सहज ही लगा लिया जाता है, फिर भी अहंता का उन्माद, विडम्बनाएँ रचने से बाज आता नहीं है।
यह तो सामान्य लोगों की बात हुई। अब प्रसंग उन विशिष्ट लोगों का आता है जो कि आदर्शवादी, त्यागी, अध्यात्मवादी, योगी, लोकसेवी आदि के रूप में प्रख्यात हैं। विशेषण करने पर इनके भीतर भी अहंता का चोर दरवाजे से घुसा और तानाशाह की तरह सहासनारूढ़ बना बैठा दिखाई पड़ता है। संतों के अखाड़े, धर्म, सम्प्रदाय, संस्था, संगठन, बड़ों की इसी प्रतिस्पर्धा में कलह के केन्द्र बने रहते हैं, उनके संचालकों में से कौन बड़ा कहलाए ? एक ही संस्था के सदस्य, एक ही लक्ष्य की दुहाई देने वाले आखिर इस कदर लड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने में निरत क्यों हैं? इसका वास्तविक कारण सामान्य लोगों की समझ से बाहर होता है, उन्हें तो कुछ भी कहकर बहका दिया जाता है। वास्तविकता इतनी भर होती है कि वे येन- केन प्रकारेण अपना बड़प्पन सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा जब आड़े आता है, तो मुहल्ले के कुत्तों की तरह अकारण एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। संगठनों के सर्वनाश में एक मात्र नहीं तो सर्वप्रधान कारण इस अहंता रूपी सूर्पणखा को ही माना जाएगा। मनोमालिन्य और विग्रह के बहाने तो सिद्धान्तवाद की दुहाई देते हुए कुछ भी गढ़े जा सकते हैं, पर यदि भारी बाँध में दरार पड़ने का कारण ढूँढ़ने के लिए गहराई तक उतरा जाय, तो प्रतीत होगा कि अहंता की नन्ही- सी चुहिया ही दुम उठाये, मुँह मटकाती, पंजे दिखाती अपनी करतूत का करिश्मा दिखा रही है ।
व्यवसाय और बच्चों को छोड़कर आने वालों से भी अहंता नहीं छूटती। जिस प्रकार कोई लालची मनोभूमि का मनुष्य भिक्षा- व्यवसाय करके पेट भरने पर भी लगातार कमाता जोड़ता रहता है और मरते समय चिथड़े तथा कुल्हड़ों में लाखों की दौलत छोड़ जाता है, उसी प्रकार लोकसेवी, अध्यात्मवादी का कलेवर बना लेने पर भी यदि अहंता न छूटी तो पैर पुजाने के लिए अनेकानेक पाखण्ड रचते, लोगों को ठगते उलझाते हुए उसे देखा जाएगा। आये दिन कुछ करतूतें, चमत्कारों की डींग हाँकते तथा और भी न जाने उसे क्या- क्या करते देखा जायेगा। सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों का घुस पड़ना वस्तुतः संगठन के लिए एक प्रकार से अभिशाप ही सिद्ध होता है। वे जितना जनहित करते हैं, उसकी तुलना में हजार गुना अनर्थ करके रख देते हैं। इसलिए उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए मनीषियों ने वित्तैषणा ( लोभ ), पुत्रैषणा (मोह) और लोकेषणा (अहंकार- बड़प्पन) की विविध एषणाओं का परित्याग करने के उपरान्त ही श्रेय मार्ग पर पैर बढ़ाने की सलाह दी है। लोकसेवी में नम्रता निरहंकारिता उत्पन्न करने के लिए प्राचीनकाल में दरवाजे- दरवाजे भिक्षा माँगने के लिए जाना पड़ता था। यों घर बैठे भी भोजन मिलने का प्रबन्ध ऐसे लोगों के लिए कठिन नहीं है, पर अहंकार गलाने का तो कोई न कोई स्वरूप चाहिए ही, इसके बिना साधु कैसा? ब्राह्मण कैसा? लोकसेवी कैसा?
गाँधी जी के आश्रम में, निवासियों को टट्टी साफ करने, झाड़ू लगाने जैसे छोटे समझे जाने वाले कार्य परिपूर्ण श्रद्धा और तत्परता के साथ करने पड़ते थे। प्रज्ञा मिशन की परम्परा भी यही है। प्रत्येक आश्रमवासी को श्रमदान अनिवार्यतः करना पड़ता है और उसमें नाली साफ करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा ढोने जैसे कार्य ही करने होते हैं ।
कई व्यक्ति सोचते हैं- हम संस्था से निर्वाह लेकर काम क्यों करें? ‘ अपना खाने ’ के नाम पर निर्वाह लेने वालों से श्रेष्ठ क्यों न बनें? कुछ लोग इस कारण काम ही नहीं करते। इस असमंजस के पीछे कोई सिद्धान्त काम नहीं करता है मात्र अहंकार ही उछलता है। हजार रुपये मासिक का काम करके यदि कोई सौ रु लेता है तो उसका नौ सौ रुपये का अनुदान ही हुआ। शान्तिकुञ्ज परम्परा में हर आश्रमवासी को अन्य सभी की तरह निर्वाह आश्रम से ही लेना पड़ता है। उसकी निजी आमदनी या पेन्शन को, उसे आश्रम में दान देते रहने के लिए कहा जाता है। लोकसेवी यदि जनता से ब्राह्मणोचित निर्वाह लेता है, तो वह वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो जाता, वरन् श्रद्धासिक्त निर्वाह दक्षिणा के रूप में प्राप्त करते हुए गौरवान्वित होता है। सच्चे सेवक के लिए ऐसी नम्रता आवश्यक है।
यहाँ एक और प्रकरण ध्यान देने योग्य है। वह है ऐसे व्यक्तियों से बचना, जो कालनेमि की तरह सतत अपना षड्यंत्र रचते व लोकसेवी की प्रगति के मार्ग में रोड़ा बनते हैं। इस प्रकार अनेकों तरह के व्यक्ति हैं। कोई सत्परामर्श देकर मनोबल ऊँचा उठाते व साधना क्षेत्र में सहयोगी बनते हैं, किन्तु आज बाहुल्य ऐसे व्यक्तियों का है जो मायावी कालनेमि की भूमिका निभाते अच्छे भले आदमी को पथ भ्रष्ट कर देते हैं।
हर समाज सेवी संस्था को ऐसे कालनेमियों से बचना पड़ता है। रावण के भाई कालनेमि का अपने काले कारनामों के कारण पुराण- कथाओं में बहुत स्थानों पर वर्णन आया है। वह त्रेता में आया था, पर काल से बद्ध नहीं था। दुर्बुद्धि देने का काम वह हर युग में करता आया है। उसी ने सूर्पणखा को नाक- कान कटाने राम के पास भेजा, रावण को सीता हरने की सलाह दी। मारीच, कुम्भकरण, मंथरा, कैकेयी की बुद्धि उलटने के मूल में उसकी ही भूमिका थी। उस कालनेमि की कुटिलता अभी भी अपना कुचक्र रचने में लगी हुई है। तपस्वी, योगी, महात्मा कोई भी वेश धारण कर उसकी विक्षुब्ध जीवात्मा सतत भटकती एवं कमजोर मनःस्थिति वाले व्यक्तियों को ढूँढ़ती रहती है। युगशिल्पियों- प्रज्ञापरिजनों को लोभ, मोह, अहंता इन तीन के अतिरिक्त कालनेमि परम्परा के व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए।
बहुत से कारण हैं जिनमें सेवा कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाती। लोग या तो गलत बातों को सही समझ कर विचलित हो जाते हैं अथवा सफलता का अहंकार उन्हें दिग्भ्रांत कर देता है। इन सब बाधाओं और भटकाव की परिस्थितियों को पहले से जान समझकर चला जाए, तो सेवाधर्म का निर्वाह, पालन किया जा सकता है। होता यह भी है कि सेवा धर्म अपना लेने के बाद उसे अपना जीवन लक्ष्य बनाने तथा उसे साधना स्तर पर करने में भूल हो जाती है। भूलें स्वभावगत हों या परिस्थितियों के कारण, लोक सेवी को उसके साधना पथ से दूर हटाती हैं ।
हमें यह तथ्य स्मरण रखना चाहिये कि मार्गदर्शक बनना हो, तो नेतृत्त्व का कौशल नहीं चरित्र चाहिए। प्राचीनकाल में लोकमानस के परिष्कार का महान् कार्य जो लोग हाथ में लेते थे, वे कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व ब्राह्मणों जैसी संयमशीलता और साधु जैसी उदार आत्मीयता का अभ्यास करते थे। इस परीक्षा में वे जितनी ऊँची कक्षा उत्तीर्ण करते थे, उसी अनुपात से उनकी सेवा- साधना सफल होती थी । यदि सच्चे मन से उच्चस्तरीय दृष्टिकोण लेकर सेवाधर्म अपनाया जाय, तो उसका परिणाम लोक- मंगल से भी अधिक आत्मोत्कर्ष के रूप में उपलब्ध होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा परिजनों को युगशिल्पी की भूमिका निभाने के लिए अग्रसर होते समय इस बात को गिरह बाँधकर रखना है कि उन्हें अपने स्तर से, व्यक्तित्व की दृष्टि से सामान्य लोगों की तुलना में कहीं ऊँचा उठकर रहना है ।
इसके लिए क्या करना होगा? इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर्तृत्व उतना नहीं है जितना कि दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रबल अभ्यास अपनाना। सर्वविदित है कि लोभ- मोह के भव- बन्धन आदर्शवादिता के, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले के लिए हथकड़ी- बेड़ियाँ जैसे अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची, संग्रही, विलासी व्यक्ति को लाभ लिप्सा इस कदर जकड़े रहती है कि उसे परमार्थ में कोई रस ही नहीं आता। अपनी तराजू पर अपने बाटों से तौलने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हलका। इसलिए लालच में राई- रत्ती कमी पड़ते ही वह परमार्थ से हाथ खींच लेता है और कुछ आडम्बर करता भी है, तो उतना ही जिससे कम खर्च में लोकसेवी पुण्यात्मा की अधिक ख्याति खरीदी जा सके। इसमें भी वे तोलते रहते हैं कि कितना गँवाया और कितना कमाया ।
दूसरा अवरोध है- व्यामोह। शरीर और परिवार के साथ अत्यधिक ममता जोड़ने वाले उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उचित- अनुचित कुछ भी करते रहते हैं। उन्हें यह छोटी परिधि लोक- परलोक सभी से बढ़कर प्रतीत होती है और उसी के निमित्त कोल्हू की तरह पिसते, आग की तरह जलते और बर्फ की तरह पिघलते रहते हैं। परिवार का उत्तरदायित्व निभाना, परिजनों के प्रति कर्तव्यपालन करना एक बात है और उन्हें सुविधाओं से लाद- लाद कर अनुचित दुलार से व्यक्तित्व की दृष्टि से हेय हीन बना देना सर्वथा दूसरी। मोहग्रस्त लोग दूसरी को अपनाते हैं और पहली की ओर से आँखें बन्द किए रहते हैं। इसके लिए कभी रोका झिड़का जाय कि उन पर अशर्फियाँ लुटाते रहने की तुलना में कहीं अधिक हित इसमें है कि वे श्रेष्ठ चिन्तन देने का प्रयास करें, मात्र लाड़- दुलार न दें, तो यह बात कोई मोहान्ध सुनता नहीं। पर कहे कौन किससे? ज्ञान वैराग्य की कथा कहते रहने वाले ही जब श्रोता भक्तजनों से भी अधिक गए- गुजरे सिद्ध होते हों, तो ‘ सत्य वचन, महाराज ’ की विडम्बना ही सिर हिलाती रहेगी।
परिवार पोषण किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नयी दृष्टि से देखने से इस परिकर के कितने ही सदस्य ऐसे होते हैं, जिनमें आर्थिक स्वावलम्बन की ही नहीं, दूसरों को सहारा देने की भी क्षमता है, किन्तु उन्हें मोहवश अथवा नाक कटने के डर से अपंग अपाहिज बनाकर रखा गया है। एक कमाऊ व्यक्ति ही मरता- खपता रहता है, दूसरे समर्थ होते हुए भी असमर्थों की विरादरी में आलसी, प्रमादी बनें बैठे रहते हैं। इसी प्रकार फिजूल खर्ची की आदतें जब अभ्यास में आ जाती हैं तो खर्च का ढोल इतना भारी हो जाता है कि उसे भी परिपोषण की संज्ञा मिलती है, वस्तुतः यह होता परिवार पोषण भर है। पोषण सरल है, तोषण अति कठिन है। पुत्रवधू की गोद से छीन- छीन कर पोते- पोतियों को कंधे पर लादे फिरने वाले बुड्ढों की भी कमी नहीं। कमाऊ लड़कों के गुलछर्रे उड़ाने में कोई कमी न रहने पर भी बुड्ढा जब उन्हीं के हाथ में पेन्शन थमाता जाता है, तो उसकी ‘ दयालुता ’ देखते ही बनती है। जीवन भर की कमाई का बँटवारा जब समर्थ बेटों की हिस्सेदारी के रूप में कर दिया जाता है, तो प्रतीत होता है कि घिनौना व्यामोह किस प्रकार औचित्य एवं प्रचलन का लबादा ओढ़कर अपने को निर्दोष सिद्ध करता है ।
इस चक्रव्यूह के कुछ थोड़े से घेरे ही यहाँ उजागर किये हैं। ऐसे- ऐसे और भी अनेकों हैं, जिनमें आये दिन बच्चे जनने, उस पर खुशी मनाने और सिर पर पर्वतों जैसे बोझ बढ़ाते चलने की भी एक बात सम्मिलित की जा सकती है। इस मोह ग्रस्तता को परमार्थ पथ पर अड़ी हुई भारी चट्टान कह सकते हैं। लोभ को प्रथम नम्बर दिया जाता है मोह को दूसरा, पर अभी यह तय किया जाना है कि इनमें से कौन द्वितीय है, वस्तुतः यह रावण, अहिरावण जैसे सगे भाई प्रतीत होते हैं ।
आत्म- कल्याण और लोक- कल्याण की साधना में ऐसा कुछ नहीं, जिसके लिए शरीर निर्वाह एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने में कोई बाधा पड़ती हो। मात्र लोभ और मोह का मद्यपों जैसा अतिवाद ही एक मात्र अवरोध है जो वस्तुतः तिनके जैसा हलका होते हुए भी पर्वत जैसा भारी बनकर दिग्भ्रान्तों के मनःक्षेत्र पर भूत- पिशाच की तरह चढ़ बैठता है और भली- चंगी परिस्थिति होते हुए भी नारकीय उत्पीड़नों की तरह निरन्तर संत्रस्त करता रहता है । किन्तु बात इतनी छोटी है नहीं। इस मार्ग में एक और बड़ा अवरोध ‘ अहंता ’ का है। यह परोक्ष होती है। न अपनी पकड़ में आती है, न दूसरों की परख में। इसलिए उसकी उखाड़- पछाड़ भी नहीं होती। फलतः मजे में अपने कोंतर में बैठी पोषण पाती, जोंक की तरह मोटी होती रहती है। इसकी विनाश लीला इतनी बड़ी है जिसकी तुलना में लोभ- मोह से होने वाली हानि को नगण्य जितना ठहराया जा सकता है ।
अहंता बड़प्पन पाने की आकांक्षा को कहते हैं। दूसरों की तुलना में अपने को अधिक महत्त्व, गौरव, श्रेय, पद, सम्मान मिलना चाहिए। यही है अहंता की आकांक्षा। इस जादूगरनी द्वारा लोगों को चित्र- विचित्र विडम्बनाएँ रचते देखा जा सकता है। केश, वस्त्र, आभूषण, सौन्दर्य प्रसाधनों की इन दिनों धूम है। फैशन के नाम पर कितना धन और कितना समय नष्ट होता है, उसे शरीर सज्जा में रुचि रखने वाले सभी जानते हैं। उस महँगे जंजाल को इसलिए रचना पड़ता है कि अहंता अपने को सुन्दर, युवा, आकर्षक, सभ्य, अमीर, सिद्ध करने के लिए इस लबादे को ओढ़कर वस्तुस्थिति से भिन्न प्रकार का प्रदर्शन करने को बाधित करती है। इसके बाद ठाट- बाट का नम्बर आता है। इसमें अमीरी का प्रदर्शन है। निवास, फर्नीचर, वाहन, नौकर तथा विलासिता के उपकरणों का सरंजाम जुटाने तथा रख- रखाव में इतना धन तथा मनोयोग लगता है, जो वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अनेक गुना मँहगा होता है। बात- बात में फिजूलखर्ची उस समय की जाती है जब उसे लोग देखें और अनुमान लगायें कि यह व्यक्ति धन कुबेर है और अनावश्यक खर्चने से भी इसे कोई कमी नहीं पड़ती। बड़प्पन पाने की मृगतृष्णा में लोग कितने पाखण्ड रचते, धन को पानी की तरह बहाने के उपरान्त आवश्यक प्रयोजनों में किस प्रकार कटौती करते हैं- इसे देखकर कोई सूक्ष्मदर्शी आश्चर्यचकित ही रह सकता है। असलियत का अनुमान सहज ही लगा लिया जाता है, फिर भी अहंता का उन्माद, विडम्बनाएँ रचने से बाज आता नहीं है।
यह तो सामान्य लोगों की बात हुई। अब प्रसंग उन विशिष्ट लोगों का आता है जो कि आदर्शवादी, त्यागी, अध्यात्मवादी, योगी, लोकसेवी आदि के रूप में प्रख्यात हैं। विशेषण करने पर इनके भीतर भी अहंता का चोर दरवाजे से घुसा और तानाशाह की तरह सहासनारूढ़ बना बैठा दिखाई पड़ता है। संतों के अखाड़े, धर्म, सम्प्रदाय, संस्था, संगठन, बड़ों की इसी प्रतिस्पर्धा में कलह के केन्द्र बने रहते हैं, उनके संचालकों में से कौन बड़ा कहलाए ? एक ही संस्था के सदस्य, एक ही लक्ष्य की दुहाई देने वाले आखिर इस कदर लड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने में निरत क्यों हैं? इसका वास्तविक कारण सामान्य लोगों की समझ से बाहर होता है, उन्हें तो कुछ भी कहकर बहका दिया जाता है। वास्तविकता इतनी भर होती है कि वे येन- केन प्रकारेण अपना बड़प्पन सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा जब आड़े आता है, तो मुहल्ले के कुत्तों की तरह अकारण एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। संगठनों के सर्वनाश में एक मात्र नहीं तो सर्वप्रधान कारण इस अहंता रूपी सूर्पणखा को ही माना जाएगा। मनोमालिन्य और विग्रह के बहाने तो सिद्धान्तवाद की दुहाई देते हुए कुछ भी गढ़े जा सकते हैं, पर यदि भारी बाँध में दरार पड़ने का कारण ढूँढ़ने के लिए गहराई तक उतरा जाय, तो प्रतीत होगा कि अहंता की नन्ही- सी चुहिया ही दुम उठाये, मुँह मटकाती, पंजे दिखाती अपनी करतूत का करिश्मा दिखा रही है ।
व्यवसाय और बच्चों को छोड़कर आने वालों से भी अहंता नहीं छूटती। जिस प्रकार कोई लालची मनोभूमि का मनुष्य भिक्षा- व्यवसाय करके पेट भरने पर भी लगातार कमाता जोड़ता रहता है और मरते समय चिथड़े तथा कुल्हड़ों में लाखों की दौलत छोड़ जाता है, उसी प्रकार लोकसेवी, अध्यात्मवादी का कलेवर बना लेने पर भी यदि अहंता न छूटी तो पैर पुजाने के लिए अनेकानेक पाखण्ड रचते, लोगों को ठगते उलझाते हुए उसे देखा जाएगा। आये दिन कुछ करतूतें, चमत्कारों की डींग हाँकते तथा और भी न जाने उसे क्या- क्या करते देखा जायेगा। सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों का घुस पड़ना वस्तुतः संगठन के लिए एक प्रकार से अभिशाप ही सिद्ध होता है। वे जितना जनहित करते हैं, उसकी तुलना में हजार गुना अनर्थ करके रख देते हैं। इसलिए उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए मनीषियों ने वित्तैषणा ( लोभ ), पुत्रैषणा (मोह) और लोकेषणा (अहंकार- बड़प्पन) की विविध एषणाओं का परित्याग करने के उपरान्त ही श्रेय मार्ग पर पैर बढ़ाने की सलाह दी है। लोकसेवी में नम्रता निरहंकारिता उत्पन्न करने के लिए प्राचीनकाल में दरवाजे- दरवाजे भिक्षा माँगने के लिए जाना पड़ता था। यों घर बैठे भी भोजन मिलने का प्रबन्ध ऐसे लोगों के लिए कठिन नहीं है, पर अहंकार गलाने का तो कोई न कोई स्वरूप चाहिए ही, इसके बिना साधु कैसा? ब्राह्मण कैसा? लोकसेवी कैसा?
गाँधी जी के आश्रम में, निवासियों को टट्टी साफ करने, झाड़ू लगाने जैसे छोटे समझे जाने वाले कार्य परिपूर्ण श्रद्धा और तत्परता के साथ करने पड़ते थे। प्रज्ञा मिशन की परम्परा भी यही है। प्रत्येक आश्रमवासी को श्रमदान अनिवार्यतः करना पड़ता है और उसमें नाली साफ करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा ढोने जैसे कार्य ही करने होते हैं ।
कई व्यक्ति सोचते हैं- हम संस्था से निर्वाह लेकर काम क्यों करें? ‘ अपना खाने ’ के नाम पर निर्वाह लेने वालों से श्रेष्ठ क्यों न बनें? कुछ लोग इस कारण काम ही नहीं करते। इस असमंजस के पीछे कोई सिद्धान्त काम नहीं करता है मात्र अहंकार ही उछलता है। हजार रुपये मासिक का काम करके यदि कोई सौ रु लेता है तो उसका नौ सौ रुपये का अनुदान ही हुआ। शान्तिकुञ्ज परम्परा में हर आश्रमवासी को अन्य सभी की तरह निर्वाह आश्रम से ही लेना पड़ता है। उसकी निजी आमदनी या पेन्शन को, उसे आश्रम में दान देते रहने के लिए कहा जाता है। लोकसेवी यदि जनता से ब्राह्मणोचित निर्वाह लेता है, तो वह वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो जाता, वरन् श्रद्धासिक्त निर्वाह दक्षिणा के रूप में प्राप्त करते हुए गौरवान्वित होता है। सच्चे सेवक के लिए ऐसी नम्रता आवश्यक है।
यहाँ एक और प्रकरण ध्यान देने योग्य है। वह है ऐसे व्यक्तियों से बचना, जो कालनेमि की तरह सतत अपना षड्यंत्र रचते व लोकसेवी की प्रगति के मार्ग में रोड़ा बनते हैं। इस प्रकार अनेकों तरह के व्यक्ति हैं। कोई सत्परामर्श देकर मनोबल ऊँचा उठाते व साधना क्षेत्र में सहयोगी बनते हैं, किन्तु आज बाहुल्य ऐसे व्यक्तियों का है जो मायावी कालनेमि की भूमिका निभाते अच्छे भले आदमी को पथ भ्रष्ट कर देते हैं।
हर समाज सेवी संस्था को ऐसे कालनेमियों से बचना पड़ता है। रावण के भाई कालनेमि का अपने काले कारनामों के कारण पुराण- कथाओं में बहुत स्थानों पर वर्णन आया है। वह त्रेता में आया था, पर काल से बद्ध नहीं था। दुर्बुद्धि देने का काम वह हर युग में करता आया है। उसी ने सूर्पणखा को नाक- कान कटाने राम के पास भेजा, रावण को सीता हरने की सलाह दी। मारीच, कुम्भकरण, मंथरा, कैकेयी की बुद्धि उलटने के मूल में उसकी ही भूमिका थी। उस कालनेमि की कुटिलता अभी भी अपना कुचक्र रचने में लगी हुई है। तपस्वी, योगी, महात्मा कोई भी वेश धारण कर उसकी विक्षुब्ध जीवात्मा सतत भटकती एवं कमजोर मनःस्थिति वाले व्यक्तियों को ढूँढ़ती रहती है। युगशिल्पियों- प्रज्ञापरिजनों को लोभ, मोह, अहंता इन तीन के अतिरिक्त कालनेमि परम्परा के व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए।
Versions
-
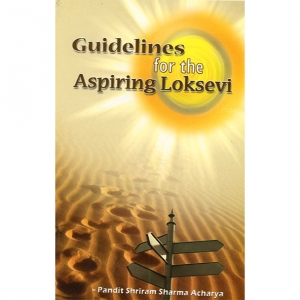
ENGLISHGuidlines for Aspiring LokseviScan Book Version
-
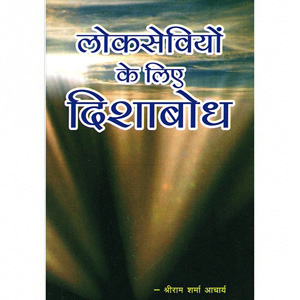
HINDIलोक सेवियो के लिये दिशा बोधScan Book Version
-
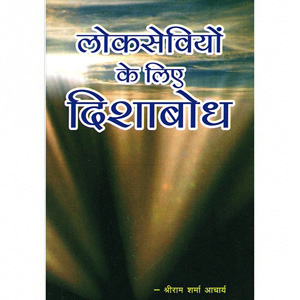
HINDIलोक सेवियों के लिए दिशाबोधScan Book Version
-
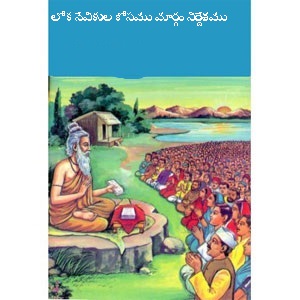
TELUGUలోక సేవికుల కోసము మార్గం నిర్దేశముScan Book Version
-
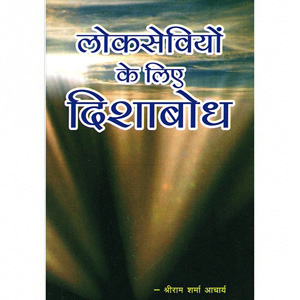
HINDIलोकसेवियों के लिए दिशाबोधText Book Version
-
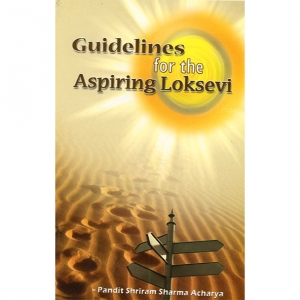
ENGLISHGuidlines for Aspiring LokseviText Book Version
Write Your Comments Here:
- विदाई की घड़ियों में उभरी पूज्य गुरुदेव की भाव संवेदना -
- अपने अंग अवयवों से
- प्रज्ञा परिजनों के सप्त महाव्रत
- जन सम्पर्क के कुछ सामान्य अनुशासन
- युग शिल्पी अहमन्यता के विषपान से बचे रहें -
- अध्यात्म क्षेत्र की वरिष्ठता विनम्रता पर निर्भर -
- दृष्टिकोण कैसा हो ?
- साधना समर के लिए समर्थ बने सृजन सैनिक
- प्रामाणिकता
- सेवा धर्म के मार्ग में बाधाएँ और भटकाव
- जीवन नीति
- आचरण और व्यवहार
- लोक व्यवहार
- सात प्रतिबन्ध

