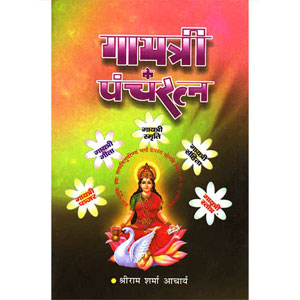गायत्री के पाँच-रत्न 
गायत्री स्मृति
Read Scan Versionॐ भूर्भुवः स्वः
भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमोम्ब्रह्मतेषु हि।
स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वेत्ति विचक्षणः ।।1।।
स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वेत्ति विचक्षणः ।।1।।
भूः भुवः और स्वः ये तीन लोक हैं, उन तीनों लोकों में ॐ ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान् उस ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में ज्ञानी है।
परमात्मा का वैदिक नाम ‘ॐ’ है। यह ‘ॐ’ तीनों लोकों में व्याप्त है। भूः पृथ्वी, भुवः पाताल, स्वः स्वर्ग—ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण हैं। भूः शरीर, भुवः संसार, स्वः आत्मा यह तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा-स्थल हैं। इन सभी स्थलों को, निखिल ब्रह्माण्ड को भगवान् का विराट् रूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो गीता के 11 वे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट् रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी। परमात्मा को सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वात्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने से परमानन्द सुख में निमग्न रहता है। ॐ भूर्भुवः स्वः का तत्वज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन-मुक्त ही हो जाता है।
तन्—तत्वज्ञास्तु विद्वांसों ब्रह्णाः स्वतपोबलैः ।
अन्धकारमपाकुर्यु र्लोकादज्ञानसम्भवम् ।।1।।
अन्धकारमपाकुर्यु र्लोकादज्ञानसम्भवम् ।।1।।
तत्त्वदर्शी विद्वान् ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से, अज्ञान द्वारा उत्पन्न अन्धकार को दूर करें।
ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता के परिणाम को देखते हैं। जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा साहित्य, शिल्पकला, विद्वान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य, आनन्द और साफल्य प्राप्त करने की ‘विद्या’ भी सीखी है। शिक्षित तो गली-कूंचियों में मक्खी-मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर जो विद्वान् हैं, वे ही ब्राह्मण हैं।
भगवान् ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान् बनने की सुविधा एवं प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिये क्योंकि वे सबसे बड़े धनी हैं।
ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भण्डार बढ़िया, कीमती, मजबूत तिजोरी में रक्खा जाता है। जो शरीर तपःपूत है, तपस्या की, संयम की, तितीक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा-तपा कर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मण रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी तपोविहीन हैं, वे शास्त्रों की तोता-रटन्त भले ही करते रहें पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए ब्राह्मण को, सद्ज्ञान के धनी को, अपने को तपःपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगन्ध की उक्ति चरितार्थ होती है।
ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे। ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भण्डारों में भरा हुआ है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुःख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुःखों का कारण और कोई नहीं है। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण-क्रन्दन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिये बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अन्धकार में भटकते हुए जन-समूह को सच्चा ब्राह्मण, अपनी सद्ज्ञान सम्पदा से लाभ पहुंचाता है। यह कर्त्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। यह ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है।
गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व की इस महान् जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। जिसकी आत्मा, जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान् और तपस्वी है, वह उतने ही अंश में ब्राह्मण है। यह ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है, उसी का यह कर्त्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अन्धकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो, अवश्य करता रहे।
स—सत्तावन्तस्तया शूराः क्षत्रियाः लोक रक्षकाः ।
आयायाशक्तिसम्भूतान् ध्वंसयेयुर्हि त्वापदः ।।3।।
आयायाशक्तिसम्भूतान् ध्वंसयेयुर्हि त्वापदः ।।3।।
सत्तावान् वीर संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें।
जन-बल, शरीर बल, सत्ता-शक्ति, पद-शासन गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस, शौर्य यह क्षत्रियत्व के लक्षण हैं। जिसके पास इन वस्तुओं में से जितनी अधिक मात्रा है, उतने ही अंशों में उसका क्षत्रियत्व बढ़ा हुआ है।
देखा गया है कि यह क्षत्रियत्व जब अनधिकारियों के हाथ में पहुंच जाता है तो इससे उन्हें अहंकार और मद बढ़ जाता है। अहंकार को बड़प्पन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च और आडम्बर बढ़ाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण द्वारा पूरी करते हैं, दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती है और इन्द्रिय-लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी दशा में वह क्षत्रियत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकारी, दम्भी, अत्याचारी, व्यसनी और कदाचारी बना देता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही उचित है।
गायत्री का ‘स’ अक्षर कहता है कि हे सत्तावानो! तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयत्न करते हैं उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। उसका उपयोग इसी में होना चाहिए।
वि—वित्तशक्त्या तु कर्त्तव्या उचिताभावपूर्तयः ।
न तु शक्त्या तया कार्य दपौद्धत्यप्रदर्शनम् ।।3।।
न तु शक्त्या तया कार्य दपौद्धत्यप्रदर्शनम् ।।3।।
धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। उस शक्ति द्वारा घमण्ड और उद्दण्डता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए और सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसलिए उसे कमाया जाना चाहिए।
पर कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होना उनकी दृष्टि में कोई ‘बहुत बड़ी बात’ होती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। इसलिए जैसे भी बने धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है। इसके लिए वे धर्म-अधर्म का, उचित-अनुचित का विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनकी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक-सेवा, ईश्वराराधना आदि सभी उपयोगी दिशाओं से वे मुंह मोड़ लेते हैं। धनपतियों को एक प्रकार का नशा-सा चढ़ा रहता है, जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत्-असत् परीक्षणी प्रज्ञा कुण्ठित हो जाती है। धनोपार्जन की यह दशा निन्दनीय है।
धन कमाना आवश्यक है, इसलिये कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सकें इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमावे, गायत्री का ‘वि’ अक्षर वित्त (धन) के सम्बन्ध में यही संकेत करता है।
तु—तुषाराणां प्रपातेऽपि यत्नो धर्मेतु चात्मनः ।
महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता पारिश्रमस्य हि ।।4।।
महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता पारिश्रमस्य हि ।।4।।
तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है।
मनुष्य जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां भी आती रहती हैं। जैसे रात और दिन समय के दो पहलू हैं वैसे ही सम्पदा और विपदा, सुख और दुःख भी जीवन-रथ के दो पहिये हैं। दोनों के लिये ही मनुष्य को धैर्य पूर्वक तैयार करना चाहिए। न विपत्ति में छाती पीटे और न सम्पत्ति में इतराकर तिरछा चले।
कठिन समय में मनुष्य के चार साथी हैं—(1) विवेक, (2) धैर्य, (3) साहस, (4) प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे-धीरे निकल जाते हैं और जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों को उपहार में दे जाते हैं। चाकू, पत्थर पर घिसे जाने पर तेज होता है, सोना अग्नि में पड़कर खरा सिद्ध होता है, मनुष्य कठिनाइयों में पड़कर इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितनी कि दश गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए कष्ट से डरना नहीं चाहिए वरन् उपर्युक्त चार साधनों द्वारा संघर्ष करके उसे परास्त करना चाहिए।
परिश्रम, प्रयत्न कर्त्तव्य, ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले, अव्यावहारिक मनुष्य प्रायः सदा ही असफल होते रहते हैं। जो कठिनाइयों पर विजयी होना और आनन्दमय जीवन का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री मन्त्र का ‘तु’ अक्षर उपदेश करता है कि प्रयत्न करो, कर्त्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थ की महिमा अपार है। ‘पुरुष’ कहाने का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है।
वि—वर नारीं बिना कोऽन्यो निर्माता मनुसन्ततेः ।
महत्त्वं रचनाशक्तेः स्वस्याः नार्यां हि ज्ञायाताम् ।।5।।
महत्त्वं रचनाशक्तेः स्वस्याः नार्यां हि ज्ञायाताम् ।।5।।
नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है अर्थात् मनुष्य की निर्मात्री नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए।
जन समाज दो भागों में बंटा हुआ है। (1) नर (2) नारी। नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया जाता है परन्तु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा एक छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा, दूसरा बहुत छोटा जुता हो, उसके द्वारा सन्तोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, हमारा समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि नारी को भी नर के समान ही अपनी क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो।
नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक ही आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद निमित्त ही होती है बाकी बालक से सब अंग-प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्थिरता, प्रतिभा, विचारधारा होगी उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूप-मण्डूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना है तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी।
गायत्री का ‘व’ अक्षर कहता है कि यदि मनुष्य-जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभायुक्त सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर-समुदाय में प्रबलता, सूक्ष्मता, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी हुई रखना अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना है।
रे—रेवेव निर्मला नारी पूजनीया सतां सदा ।
यतो हि सर्व लोकेऽस्मिन् साक्षल्लक्ष्मीमता बुधैः ।।6।।
यतो हि सर्व लोकेऽस्मिन् साक्षल्लक्ष्मीमता बुधैः ।।6।।
सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि विद्वानों ने उसको इस संसार में साक्षात् लक्ष्मी माना है।
जैसे नर्मदा नदी का जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को निर्मल अन्तःकरण दिया है। परिस्थिति दोष के कारण अथवा दुष्ट संगति से कभी-कभी उसमें विकार पैदा हो जाते हैं; पर इन कारणों को बदल दिया जाय तो नारी-हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रक्खा जाय या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाय तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगती है। परन्तु पीछे जब उन कारणों को हटा दिया जाय तो वह शुद्ध, निर्मल, शुभ मणि ही दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार नारी जब बुरी परिस्थितियों में फंसी हो तब बुरी दिखाई देती है। उस परिस्थिति का अन्त होते ही वह निर्मल एवं निर्दोष हो जाती है।
वैधव्य, किसी की मृत्यु, घाटा आदि दुर्घटनायें घटित होने पर उसे नव आगन्तुक वधू के भाग्य का दोष बताना नितान्त अनुचित है। ऐसी घटनाएं होतव्यता के अनुसार होती हैं। नारी तो लक्ष्मी का अवतार होने से सदा ही कल्याणकारिणी और मंगलमयी है। गायत्री का अक्षर ‘रे’ नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो।
ण्य—न्यसन्ते ये नराः पादान् प्रकृत्याज्ञानुसारतः ।
स्वस्थाः सन्तस्तु ते नूनं रोगमुक्ता भविन्ति हि ।।7।।
स्वस्थाः सन्तस्तु ते नूनं रोगमुक्ता भविन्ति हि ।।7।।
जो मनुष्य प्रकृति की आज्ञानुसार पैरों को रखते हैं अर्थात् प्रकृति की आज्ञानुसार चलते हैं वे मनुष्य स्वस्थ होते हुए निश्चय ही रोगों से मुक्त हो जाते हैं।
स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार-विहार अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, बनावटी, आडम्बर और विलासिता से भरा हुआ जीवन बिताने से लोग बीमार बनते हैं, और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं।
(1) भूख लगने पर खूब चबा कर प्रसन्नचित्त से, थोड़ा पेट खाली रखकर भोजन करना। (2) फल, शाक, दूध, छिलके समेत अन्न और दालें जैसे ताजे सात्विक आहार लेना। (3) नशीली चीजें, मिर्च मसाले, चाट, पकवान, मिठाइयां, मांस आदि अभक्ष्यों से बचना। (4) सामर्थ्य के अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना। (5) शरीर, वस्त्र, मकान और प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना। (6) रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना। (7) मनोरंजन, देशाटन, निर्दोष विनोद के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त करते रहना। (8) कामुकता, चटोरेपन, अन्याय, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिन्ता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारों से मन को हटाकर सदा प्रसन्नता और सात्विकता के सद्विचारों में रमण करना। (9) स्वच्छ जलवायु का सेवन। (10) उपवास, ऐनेमा, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग-मुक्ति का उपाय करना। ये दस नियम ऐसे हैं कि जिन्हें अपनाकर प्राकृतिक जीवन बिताने से खोये हुए स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं उन्नत बनाना बिल्कुल सरल है। गायत्री का ‘ण्य’ अक्षर यही उपदेश करता है।
भ—भवोद्विग्नमना नैव हृदुद्वेग परित्यज ।
कुरु सर्वव्यवस्यासु शांतं संतुलितं मनः ।।8।।
कुरु सर्वव्यवस्यासु शांतं संतुलितं मनः ।।8।।
मानसिक उत्तेजना को छोड़ दो। सभी आवश्यकताओं में मन को शान्त और सन्तुलित रखो।
शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ‘ज्वर’ कहलाता है और ज्वर अनेक दुष्परिणामों को पैदा कर सकता है जैसे ही उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मद, आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्वर के हैं। आवेश का अन्धड़ तूफान जिस समय मन में आता है उस समय ज्ञान, विचार, विवेक सबका लोप हो जाता है और उस सन्निपात से ग्रस्त व्यक्ति अंड-बंड बातें बकता है न करने लायक अस्त-व्यस्त क्रियायें करता है। वह स्थिति मानव जीवन में सर्वथा अवांछनीय है।
विपत्ति पड़ने पर लोग चिन्ता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध, कायरता आदि विषादात्मक आवेश से ग्रस्त हो जाते हैं और सम्पत्ति बढ़ने पर अहंकार, मद, मत्सर, अतिहर्ष, अमर्यादा, नास्तिकता, अतिभोग, ईर्ष्या, द्वेष आदि विध्वंसक उत्तेजनाओं में फंस जाते हैं। कई बार लोभ और भोग का आकर्षण उन्हें इतना लुभा लेता है कि आंखें रहते हुए भी अन्धे हो जाते हैं। इन तीनों स्थितियों में मनुष्य का होश-हवास दुरुस्त नहीं रहता। देखने में वह स्वस्थ और भला चंगा दीखता है पर वस्तुतः उसकी आन्तरिक स्थिति पागलों, बालकों, रोगियों तथा उन्मत्तों जैसी हो जाती है। ऐसी स्थिति मनुष्य के लिये विपत्ति, त्रास, अनिष्ट और अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए गायत्री के ‘भू’ शब्द का सन्देश है कि इन आवेशों और उत्तेजनाओं से बचो। दूरदर्शिता, विवेक, शान्ति और स्थिरता से काम लो। बदली की छाया की तरह रोज घटित होते रहने वाली रंग-बिरंगी घटनाओं से अपनी आन्तरिक शान्ति को नष्ट न होने दो। मस्तिष्क को स्वस्थ रक्खो, चित्त को शान्त रहने दो, आवेश की उत्तेजना से नहीं, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर अपनी विचारधारा और कार्य प्रणाली को चलाओ।
गो—गोप्याः स्बीया मनोवृत्तिर्नासहिष्णुनरो भवेत् ।
स्थितिमन्यस्य च वीक्ष्य तदनुरूपतां चरेत् ।।9।।
स्थितिमन्यस्य च वीक्ष्य तदनुरूपतां चरेत् ।।9।।
अपने मनोभावों को नहीं छिपाना चाहिए। मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए। दूसरे की स्थिति को देखकर उसके अनुसार आचरण करे।
अपने मनोभाव और मनोवृत्ति को छिपाना, छल, कपट और पाप है। जैसे भीतर है वैसे ही बाहर प्रकट कर दिया जाय तो वह पाप निवृत्ति का सबसे बड़ा राजमार्ग है। कोई व्यक्ति यदि अधिक रहस्यवादी हो, अधिक अपराधी कार्य करता हो तो भी वह अपने कुछ ऐसे आत्मीयजन, विश्वासी जीव अवश्य रखना चाहता है, जिनके आगे अपने सब रहस्य प्रकट करके मन हल्का कर लिया करे। ऐसे आत्मीय मित्र गुरुजन हर मनुष्य को नियुक्त कर लेने चाहिए।
प्रत्येक मनुष्य के दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार विभिन्न होते हैं। इसलिये सबको सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझते हुए दूसरों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। अपने से किसी भी अंश में मतभेद रखने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, दुराचारी या विरोधी मान लेना उचित नहीं। ऐसी असहिष्णुता झगड़ों की जड़ है। एक दूसरे के दृष्टिकोण के अन्तर को समझते हुए यथासम्भव समझौते का मार्ग निकालना चाहिए। फिर भी जो मतभेद रह जाय उसे पीछे धीरे-धीरे सुलझाते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए।
संसार में सभी प्रकृति के मनुष्य हैं। मूर्ख-विद्वान्, रोगी-स्वस्थ, पापी पुण्यात्मा, पाखंडी, कायर-वीर, कटुवादी-मृदुभाषी, चोर-ईमानदार, निन्दनीय-आदारास्पद, स्वधर्मी-विधर्मी, दया-पात्र दण्डनीय, शुष्क-सरस, भोगी-त्यागी आदि परस्पर विरोधी स्थितियों के मनुष्य भरे पड़े हैं। उनकी स्थिति को देखकर तदनुसार उनसे भाषण, व्यवहार, सहयोग करें। उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके लिए शक्य-सलाह दें। सबसे एक समान व्यवहार नहीं हो सकता और न सब एक मार्ग पर चल सकते हैं। यह सब बातें, ‘गो’ अक्षर हमें सिखाता है।
दे—देयानि स्ववशे पुंसा स्वेन्द्रियाण्यखिलानि वं ।
असंयतानि खादन्ति तान्तीन्द्रियाणि स्वामिनम् ।।10।।
असंयतानि खादन्ति तान्तीन्द्रियाणि स्वामिनम् ।।10।।
मनुष्य को अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियां अपने वश में करनी चाहिए। ये असंयत इन्द्रियां स्वामी को खाती हैं।
इन्द्रियां आत्मा के औजार हैं, घोड़े हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकता पूरी हो और सुख मिले। सभी इन्द्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का काम जीव को उत्कर्ष एवं आनन्द प्रदान करना है। यदि उसका सदुपयोग हो तो क्षण-क्षण पर मानव-जीवन का मधुर रस खता हुआ प्राणी अपने भाग्य को सराहता रहेगा।
किसी इन्द्रिय का भोग पाप नहीं है। सच तो यह है कि अन्तःकरण की विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओं को तृप्त करने का इन्द्रियां एक माध्यम है। जैसे पेट की भूख-प्यास को न बुझाने से शरीर का सन्तुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की क्षुधाएं उचित रीति से तृप्त न की जाती रहें तो आंतरिक क्षेत्र का सन्तुलन बिगड़ जाता है और अनेक मानसिक रोग उठ खड़े होते हैं।
इन्द्रिय भोगों की जगह-जगह निन्दा की जाती है और वासनाओं को दमन करने का उपदेश दिया जाता है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियन्त्रित इन्द्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न करके भी मनमानी करती हैं। आज-कल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार के इन्द्रिय-गुलाम हैं। अपनी वासना पर काबू नहीं रख सकते। बेकाबू हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है।
गायत्री का ‘दे’ अक्षर आत्म-नियंत्रण का उपदेश देता है।
व—वस नित्यं पवित्रः सन् बाह्यऽभ्यन्तरतस्तथा ।
गतः पवित्रतायां हि राजतेऽति प्रसन्नता ।।11।।
गतः पवित्रतायां हि राजतेऽति प्रसन्नता ।।11।।
मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए। क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है।
मलीनता अन्ध तामसिकता की प्रतीक है। आलस्य और दारिद्र्य, पाप और पतन जहां रहते हैं वहां मलीनता या गन्दगी का निवास होता है। जो इस प्रकृति के हैं उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गन्दगी और अस्त-व्यस्तता भरी रहती है। इसके विपरीत जहां चेतनता, जागरूकता, सुरुचि, सात्त्विकता होगी वहां सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जायगा। सफाई सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है।
मलीनता से घृणा होनी चाहिए पर उसे हटाने या उठाने में रुचि होनी चाहिए। जो गन्दगी को छूने या उसे उठाने, हटाने में हिचकिचाते हैं वे सफाई नहीं रख सकते। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गन्दगी पैदा होती है। निरन्तर टूट-फूट एवं जीर्णता के लक्षण प्रकट होते रहते हैं। यदि बार-बार जल्दी-जल्दी उस मलीनता का परिशोधन न किया जाय, टूट-फूट का जीर्णोद्धार न किया जाय, तो गन्दगी बढ़ती जायगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल एक कल्पना पात्र बनी रह जायगी।
गायत्री का ‘व’ अक्षर स्वच्छता का सन्देश देता है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ निवास, स्वच्छ सामान, स्वच्छ जीविका, स्वच्छ विचार, स्वच्छ व्यवहार, जिसमें इस प्रकार की स्वच्छतायें निवास करती हैं, वह पवित्रात्मा मनुष्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त करता है।
स्य—स्यन्दनं पदार्थो हि बुधैर्मतः ।
योऽन्यान् सुखयते विद्वान् तस्य दुःखं विनश्यति ।।12।।
योऽन्यान् सुखयते विद्वान् तस्य दुःखं विनश्यति ।।12।।
दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना परमार्थ का रथ है ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। जो विचारवान् दूसरे लोगों को सुख देता है, उसका दुःख नष्ट हो जाता है।
लोक व्यवहार के तीन मार्ग हैं—(1) अर्थ—जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से आदान-प्रदान करते हैं, (2) स्वार्थ—दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करना, (3) परमार्थ—अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाना। स्वार्थ में चोरी, ठगी, अपहरण, शोषण, बेईमानी आदि आते हैं। परमार्थ दान सेवा, सहायता, शिक्षा, आदि कार्यों को कहा जाता है।
अर्थ (जीविका) हमारा नित्यकर्म है। उसके बिना जीवन-यात्रा भी नहीं चक सकती। आहार, निद्रा, भोजन, मल त्याग आदि के समान स्वाभाविक होने के कारण उसका विधि-निषेध कुछ नहीं है। वह तो हर एक को करना ही होता है। स्वार्थ त्याज्य है, निन्दनीय है, पाप मूलक है, उससे यथासम्भव बचते ही रहना चाहिए। परमार्थ धर्म-कार्य है, इससे अपने में त्याग का, उदारता का अभ्यास बढ़ता है और आत्म-कल्याण का धर्म-मार्ग प्रशस्त होता है तथा उससे दूसरों का लाभ होने से वह प्रसन्न होकर बदले में प्रत्युपकार करते हैं, प्रशंसा तथा आदर देते हैं और कृतज्ञ रहते हैं।
गायत्री का ‘स्य’ शब्द प्रेरणा देता है कि हर मनुष्य का कर्त्तव्य है कि अर्थ उपार्जन करता हुआ स्वार्थ से बचे और परमार्थ के लिए यथा सम्भव प्रयत्नशील रहे। अपना पेट तो पशु-पक्षी भी भर लेते हैं, प्रशंसनीय वह है जिसके द्वारा दूसरे भी लाभ उठावें।
धी—धीरस्तुष्टो भजेन्नैव ह्येकस्यां हि समुन्नतौ ।
क्रियतामुन्नतिस्तेन सर्वास्वाशासु जीवने ।।13।।
क्रियतामुन्नतिस्तेन सर्वास्वाशासु जीवने ।।13।।
धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की सभी दिशाओं में उन्नति करनी चाहिए।
जैसे मनुष्य के कई अंग हैं और उन सभी का पुष्ट होना आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन की अनेक दिशायें हैं और उन सभी का विकास होना सर्वतोमुखी उन्नति का चिन्ह है। यदि पेट बहुत बढ़ जाय और हाथ-पांव पतले हो जायें तो इस विषमता से प्रसन्नता न होकर चिन्ता ही बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि कोई आदमी केवल धनी, केवल विद्वान् या केवल पहलवान बन जाय तो वह उन्नति पर्याप्त न होगी। वह पहलवान किस काम का जो दाने-दाने को मुहताज हो, वह विद्वान् किस काम का जो रोगों में ग्रस्त रहता हो, वह धनी किस काम का जिसके पास न विद्या है न तन्दुरुस्ती।
केवल एक ही दिशा में उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना और अन्य दिशाओं की उपेक्षा करना, उनकी ओर से उदासीन रहना उचित नहीं। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय आठ दिशायें हैं वैसे ही जीवन की भी आठ दिशा हैं, आठ बल हैं। (1) स्वास्थ्य-बल, (2) विद्या-बल, (3) धन-बल, (4) मित्र-बल, (5) प्रतिष्ठा-बल, (6) चातुर्य-बल, (7) साहस-बल, (8) आत्म-बल। इन आठों का यथोचित मात्रा में संचय होना चाहिए। जैसे किसान खेत को सब ओर से ठीक रखता है, जैसे चतुर सेनापति युद्ध-क्षेत्र के सब मोर्चों की रक्षा करता है, वैसे ही जीवन-युद्ध के ये आठों मोर्चे सावधानी के साथ ठीक रखे जाने चाहिए। जिधर भी भूल रह जायगी उधर से ही शत्रु का आक्रमण होने और परास्त होने का भय रहेगा।
गायत्री का ‘धी’ शब्द हमें सजग करता है कि आठों बल बढ़ाओं, आठों मोर्चों पर सजग रहो, आठों दिशाओं की रखवाली करो तभी सर्वांगीण उन्नति हो सकेगी।
म—महेश्वरस्य विज्ञाय नियमान्नयाय संयुतान् ।
तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासयेत् ।।।।
तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासयेत् ।।।।
‘‘परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें।’’
परमात्मा के नियम न्यायपूर्ण हैं। सृष्टि में उसके प्रधान कार्य भी दो ही हैं। (1) संसार को नियमबद्ध रखना, (2) कर्मों का न्यायानुकूल फल देना। इन दोनों ईश्वरीय प्रधान कार्यों को समझ कर जो अपने को नियमानुसार बनाता है, प्रकृति के कठोर नियमों को ध्यान में रखता है, सामाजिक राजकीय, धार्मिक, लोक हितकारी कानूनों, कायदों को मानता है वह एक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जो यह समझता है कि न्याय की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा और बुरे-भले कर्मों के अनुसार दुःख-सुख की प्राप्ति अनिवार्यतः होगी वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। काम करने पर ही उसकी उजरत मिलती है। जो पसीना बहायेगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ, उद्योग और चतुरता का परिचय देगा, उसे उसके प्रयत्न के अनुसार साधन सामग्री जुटाने में सफलता मिलेगी।
परमात्मा की पूजा-उपासना की जितनी साधनायें है, जितने कर्मकाण्ड हैं, उनका तात्पर्य यही है कि साधक परमात्मा के अस्तित्व पर उसकी सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता पर विश्वास करे। यह विश्वास जितना ही दृढ़ होगा, उतना ही उसे परमात्मा का नियम और न्याय स्मरण रहेगा। इन दोनों की कठोरता और निश्चिन्तता पर विश्वास होना, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का हेतु है। जो समझता है कि शीघ्र या देर-सवेर में तुरन्त या विलम्ब से, कर्म का फल मिले बिना नहीं रह सकता, वह आलसी या कुकर्मी नहीं हो सकता। जो आलस्य और कुकर्म से जितना बचता है वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है। गायत्री का ‘म’ अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है। बताता है कि ईश्वरीय नियम और न्याय का ध्यान रखते हुए हम सत्पथ पर चलें।
हि—हितं मत्वा ज्ञानकेन्द्रं स्वातंत्र्येण विचारयेत् ।
नान्धानुसरणं कुर्यात् कदाचित् कोऽपि कस्यचित् ।।15।।
नान्धानुसरणं कुर्यात् कदाचित् कोऽपि कस्यचित् ।।15।।
‘हितकारी ज्ञान केन्द्र को समझकर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करे। कभी भी कोई किसी का अन्धानुसरण न करे।’
देश, काल, पात्र, अधिकार और परिस्थिति के अनुसार मानव-जाति के हल और सुविधा के लिए विविध प्रकार के नियम, धर्मादेश, कानून और प्रथाओं का निर्माण एवं परिचालन होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ इन प्रथाओं एवं मान्यताओं का परिवर्तन होता रहता है।
समाज के सुसंचालन के लिए प्रथायें हैं। मनुष्य जाति की सुव्यवस्था के लिए उन्हें बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उन प्रथाओं को अपरिवर्तनशील समझकर समाज और जाति के लिए उन्हें अमिट लकीर मान लिया जाय। संसार में आदि काल से बराबर परिवर्तन होता आ रहा है। कई रिवाजें आज के लिए अनुपयुक्त हैं तो ऐसा नहीं कि परम्परा मोह के कारण उनका अन्धानुकरण किया ही जाय।
गायत्री का ‘हि’ अक्षर कहता है कि मनुष्य समाज के हित का ध्यान रखते हुए देश, काल और विवेक के अनुसार प्रथाओं को, परम्पराओं को बदला जा सकता है। आज हिन्दू समाज में ऐसी अगणित प्रथायें प्रचलित हैं जिन्हें बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है।
धि—धिया मृत्युं स्मरन् मर्म जानीयाज्जीवनस्य च ।
तदा लक्ष्य समालक्ष्य पादौ संततमाक्षिपेत् ।।16।।
तदा लक्ष्य समालक्ष्य पादौ संततमाक्षिपेत् ।।16।।
‘बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखे और जीवन के मर्म को समझे तब अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर अपने पैरों को चलावें अर्थात् निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े।’
जीवन और मृत्यु के रहस्य को विवेक पूर्वक गम्भीरता से समझना आवश्यक है। मृत्यु से कोई डरने की बात नहीं, पर उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। न जाने किस समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो और कूच की तैयारी करनी पड़े। इसलिए जो समय हाथ में है, उसे अच्छे से अच्छे उपयोग में लगाना चाहिए। धन, यौवन आदि अस्थिर हैं। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है, इसलिए इनका अहंकार न करके, दुरुपयोग न करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे भावी जीवन में सुख-शान्ति की अभिवृद्धि हो।
जीवन एक अभिनय है और मृत्यु उसका पटाक्षेप है। इस अभिनय को हमें इस प्रकार करना चाहिए, जिससे दूसरों की प्रसन्नता बढ़े और अपनी प्रशंसा हो। नाटक या खेल के समय सुखपूर्ण और दुःख भरे अनेकों अवसर आते हैं, पर अभिनयकर्ता समझता है कि यह केवल खेल-मात्र हो रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, उस खेल के समय होने वाले दुख के अभिनय में न दुःखी होता है, न सुख के अभिनय में सुखी वरन् अपना कौशल प्रदर्शित करने में, अपनी नाट्य सफलता में प्रसन्नता अनुभव करता है। जीवन-नाटक का भी अभिनय इसी प्रकार होना चाहिए। हर समय मनुष्य पर आये दिन आने वाली सम्पदा-विपदा का कुछ महत्व नहीं, उनकी ओर विशेष ध्यान न देकर अपना कर्म-कौशल दिखाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। मृत्यु, जीवन का अन्तिम अतिथि है। उसके स्वागत के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो तो तैयारी में कोई कमी अनुभव न करनी पड़े।
गायत्री का ‘धि’ अक्षर जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाता है। जीवन को इस प्रकार बनाओ जिससे मृत्यु के समय पश्चात्ताप न हो। जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे जीवन और मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते हैं।
यो—यो धर्मो जगदाधारः स्वचारणे तमानय ।
भा विडम्बय तं सोऽस्ति ह्येको मार्गे सहायकः ।।17।।
भा विडम्बय तं सोऽस्ति ह्येको मार्गे सहायकः ।।17।।
‘जो धर्म संसार का आधार है, उस धर्म को अपने आचरण में लाओ। उनकी विडम्बना मत करो। वह तुम्हारे मार्ग में एक ही अद्वितीय सहायक है।’
धर्म संसार का आधार है। उसके ऊपर विश्व का समस्त भार रखा हुआ है। यदि धर्माचरण उठ जाय और सब लोग पूर्णरूप से अधर्मी बन जायें तो एक क्षण के लिए भी कोई प्राणी चैन से न बैठ सकेगा। सबको अपने प्राण बचाने और दूसरे का अपहरण करने की चक्की के दुहरे पाटों के बीच पिसना पड़ेगा। आज अनेक व्यक्ति लुका−छिपी कर अधर्माचरण करते हैं पर उन्हें भी यह साहस नहीं होता कि प्रत्यक्षतः अपने को अधर्मी घोषित करें या अधर्म को उचित ठहराने की वकालत करें। बुराइयां भी भलाई की आड़ लेकर की जाती हैं। इससे प्रकट है कि धर्म ऐसी मजबूत चीज है कि उसी का आश्रय लेकर, आडम्बर ओढ़कर दुष्ट दुराचारी भी अपना बेड़ा पार लगाते हैं। ऐसे मजबूत आधार को ही हमें अपना अवलम्बन बनाना चाहिए।
कई आदमी धर्म को कर्मकाण्ड का पूजन-पाठ या तीर्थ-व्रत, दान आदि का विषय मानते हैं और कुछ समय इनमें लगाकर शेष समय को नैतिक-अनैतिक कैसे ही कार्य करने के लिए स्वतन्त्र समझते हैं। यह भ्रांत धारणा है। धर्म, पूजा-पाठ तक ही सीमित रहने वाली वस्तु नहीं है। वरन् उसका उपयोग तो अपनी प्रत्येक विचार-धारा और क्रिया प्रणाली में पूरी तरह होना चाहिए।
गायत्री का ‘यों’ अक्षर बताता है कि धर्म की विडम्बना मत करो, उसे आडम्बर का आचरण मत बनाओ, वरन् उसे अपने जीवन में घुला डालो। जो कुछ सोचो, जो कुछ करो, वह धर्मानुकूल होना चाहिए। शास्त्र की उक्ति है कि—‘रक्षा किया हुआ धर्म अपनी रक्षा करता है और धर्म को जो मारता है धर्म उसे मार डालता है।’ इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें धर्म को ही अपनी जीवन नीति बनाना चाहिए।
यो—योजन व्यसनेभ्यः स्यात्तानि पुंसस्तु शत्रवः ।
मिलत्वैतानि सर्वाणि समये घ्नन्ति मानवम् ।।18।।
मिलत्वैतानि सर्वाणि समये घ्नन्ति मानवम् ।।18।।
‘व्यसनों से योजन भर दूर रहे अर्थात् व्यसनों से बचा रहे क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं।’
व्यसन मनुष्य के प्राण घातक शत्रु हैं। मादक पदार्थ व्यसनों में प्रधान हैं। तम्बाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीजें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। इनसे क्षणिक उत्तेजना आती है। जिन लोगों की जीवनी-शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है वे अपने को शिथिल तथा अशक्त अनुभव करते हैं उसका उपचार, आचार-विहार प्रकृति में अनुकूल परिवर्तन करके शक्ति संचय की वृत्ति द्वारा वर्धन होना चाहिए। परन्तु भ्रांत मनुष्य दूसरा मार्ग अपनाते हैं। वे थके घोड़े को चाबुक मार-मार कर दौड़ाने का उपक्रम करके चाबुक को शक्ति का केन्द्र मानने की भूल करते हैं। नशीली चीजें मस्तिष्क को मूर्छित कर देती हैं, जिससे मूर्छाकाल में शिथिलतावश पीड़ा नहीं होती। दूसरी ओर वे चाबुक मार मार कर उत्तेजित करने की क्रिया करती हैं। नशीली चीजों का सेवन करने वाला ऐसा समझता है कि वे मुझे बल दे रही हैं, पर वस्तुतः उनसे बल नहीं मिलता, वरन् रही बची हुई शक्तियां भड़क कर बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं और मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन-दिन क्षीण होते-होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। व्यसन मित्र के वेष में शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं।
नशीले पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। वे उनसे छोड़े नहीं छूटते। सिनेमा, नाचरंग, व्यभिचार, मुर्गा, तीतर, बटेर लड़ाना आदि कितनी ही हानिकारक और निरर्थक आदतों के शिकार बनकर लोग अपना धन, समय और स्वास्थ्य निरर्थक बर्बाद करते हैं।
गायत्री का ‘यो’ अक्षर व्यसनों से दूर रहने का आदेश करता है, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों का नाश करने वाले हैं। व्यसनी मनुष्य की वृत्तियां नीचे मार्ग की ओर ही चलती हैं।
नः—न;शण्वेकामिमां वार्तां ‘जागृतस्त्वं सदा भव’ ।
सप्रमादं नरं नूतं ह्याक्रामन्ति विपक्षिणः ।।19।।
सप्रमादं नरं नूतं ह्याक्रामन्ति विपक्षिणः ।।19।।
‘हमारी यह एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो। क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण कर देते हैं।’
असावधानी, आलस्य, बेखबरी, अदूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक आपत्तियों की जननी कह सकते हैं। बेखबर आदमी पर चारों ओर से हमले होते हैं। असावधानी में ऐसा आकर्षण है, जिससे खिंच-खिंच कर अनेक प्रकार की हानियां, विपत्तियां एकत्रित हो जाती हैं। असावधान, आलसी पुरुष एक प्रकार का अर्द्धमृत है। मरी हुई लाश को पड़ी देखकर जैसे चील, कौए, कुत्ते, श्रृंगाल, गिद्ध दूर-दूर से दौड़कर वहां जमा हो जाते हैं, वैसे ही असावधान पुरुष के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं से आकर अपनी घात लगाते हैं।
जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर-सवेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आते रहने वाले उतार-चढ़ावों से बेखबर है वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बन्द किये रहता है वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना न रहेगा। जो दुनियां के छल, फरेब, झूंठ, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं, जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता उसे दुनियां के शैतानी तत्व बुरी तरह नोंच खाते हैं।
इसलिये गायत्री का ‘न’ अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहा, जागते रहो कि तुम्हें शत्रुओं के आक्रमण का शिकार न बनना पड़े।
प्र—प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदारः कदाचन ।
चिन्तयोदार हृष्ट्यैव तेन चित्तं विशुद्धयति ।।20।।
चिन्तयोदार हृष्ट्यैव तेन चित्तं विशुद्धयति ।।20।।
‘स्वभाव से ही उदार होओ, कभी भी अनुदार मत बनो, उदार दृष्टि से ही विचार करो ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है।’