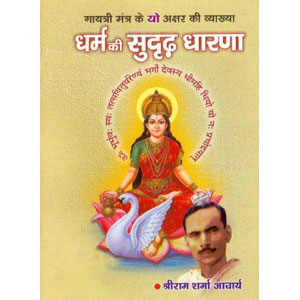धर्म की सुदृढ़ धारणा 
धर्म का व्यापक स्वरूप
Read Scan Versionनित्य व्यवहार में धर्म शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग" इसी में अर्थ किया जाता है । जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि "तेरा कौनसा धर्म है ?'' तब उससे हमारे पूँछने का यही हेतु होता है कि तू अपने पारलौकिक कल्याण के लिये किस मार्ग-वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी या पारसी से चलता है और हमारे प्रश्न के अनुसार ही वह उत्तर देता है । उसी तरह स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधनभूत, यज्ञ, योग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय ''अथातो धर्म जिज्ञासा" आदि धर्म सूत्रों में भी धर्म शब्द का यही अर्थ लिया गया है परंतु धर्म शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है । इसके सिवा राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नीति बोधकों को भी धर्म कहते हैं | धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को 'मोक्षधर्म अथवा सिर्फ मोक्ष और व्यवहारिक धर्म अथवा केबल नीति को केवल धर्म कहा करते हैं । उदाहरणार्थ चतुर्विधि पुरुषार्थों की गणना करते समय हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा करते हैं ।
महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है और जिस स्थान में कहा गया है कि 'किसी का कोई काम करना धर्म-संगत है' उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्य शास्त्र अथवा तत्कालीन समाज व्यवस्था शास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है तथा जिस स्थान में पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर मोक्ष धर्म के आशय से इसका प्रयोग किया गया है इसी प्रकार मनु आदि स्मृति ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र के विशिष्ट कर्मों अर्थात् चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन करते समय केबल धर्म अर्थ का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है । गीता में भी 'स्वधर्म मपि चावेक्ष्य (गीता २-३१) स्वधर्में निघनं श्रेय: परधर्मो भयावह:' ( ३-३५) आदि कई स्थानों पर धर्म शब्द इस लोक के चातुर्वर्ण्य के धर्म के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है ।
पुराने जमाने के ऋषियों ने श्रम विभाग रुप चातुर्वर्ण्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावें । किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पड़ने पावे और समाज का सभी दशाओं से संरक्षण और पोषण भली भांति होता रहे । यह बात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जात मात्रोपजीवी हो गये अर्थात् सच्चे स्वधर्म को भूल कर वे केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो गये ।
ऊर्ध्व बाहुर्विरौम्येष: न च कश्चिच्छ्र् णोति माम् । धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म किं न सेव्यते ।
''अरे भुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, परन्तु कोई भी नहीं सुनता धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिये इस प्रकार के धर्म का आचरण तुम क्यों नहीं करते हो ।''
क्या संस्कृत क्या अन्य कोई भाषा सभी में धर्म शब्द का प्रयोग उन सब नीति नियमों के बारे में किया गया हैं जो समाज धारा के लिये शिष्ट जनों के द्वारा अध्यात्म दृष्टि से बनाये गये हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा शिष्टाचार को धर्म की बुनियाद कह सकते हैं जो समाज धारा के लिये शिष्ट जनों के द्वारा प्रचलित किये गये हो । और इसलिये महाभारत (अनु १४०-१५७) में एवं स्मृति ग्रंथों में ''आचार प्रभवो धर्म:'' अथवा आचार: परमोधर्मः ( मनु १-१०८) अथवा धर्म को मूल बतलाते समय ''वेदः स्मृति: सदाचार: स्वस्थ प्रियमात्मन्:"(मनु १२-२) इत्यादि वचन कहे हैं ।
धर्म शब्द की दूसरी एक और व्याख्या प्राचीन ग्रंथों में दी गयी है, यह व्याख्या मीमांसकों की है । ''चोदना लक्षणाऽर्थों धर्म:"(जै. सू. १-१-२) किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा आज्ञा करना कि "तू अमुक कर" अथवा 'मत कर' 'चोदना' यानि प्रेरणा है । जब तक इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है । इसका आशय यही है कि पहले पहल निर्बन्ध या प्रबंध के कारण धर्म निर्माण हुआ । धर्म की यह व्याख्या कुछ अंश में प्रसिद्ध अंग्रेज ग्रन्थकार हाव्स के मत से मिलती है । असभ्य तथा जंगली अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण समय समय पर उत्पन्न होने वाली मनोवृत्तियों की प्रबलता के कारण हुआ करता है । परन्तु धीरे-धीरे उस समय के बाद यह मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं है और यह विश्वास होने लगता है कि इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार कार्य करने में ही सब लोगों का कल्याण है, तब प्रत्येक मनुष्य ऐसी मर्यादाओं का पालन कायदे के तौर पर करने लगता है, जो शिष्टाचार या अन्य रीति से सुदृढ़ हो जाया करती हैं । जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है । पूर्व समय में विवाह व्यवस्था का प्रचार नहीं था, पहले-पहल उसे स्वेतकेतु ने चलाया । इसी प्रकार शुक्राचार्य ने मदिरा पान को निषिद्ध ठहराया । यह न देख कर कि इन मर्यादाओं को बनाने में श्वेतकेतु अथवा शुक्राचार्य का क्या हेतु था, केवल किसी एक बात पर ध्यान देकर कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का काम या कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा धर्म शब्द की 'चोदना लक्षणोऽर्थों: धर्म:' व्याख्या बनाई गई है ।
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वश मागच्छेत् नौ ह्यस्य परि पथिनौ ।।
प्रत्येक इन्द्रिय में अपने-अपने उपयोग अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में जो प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभाव सिद्ध हैं । इनके वंश में हमें नहीं पड़ना चाहिए । क्योंकि राग और द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं । तब भगवान भी धर्म का वही लक्षण स्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर कहा गया है । मनुष्य की इद्रियाँ उसे पशु के समान आचरण करने के लिये कहा करती है और उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा में खींचा करती है । इस कलहाग्नि में जो लोग अपने शरीर में संचार करने वाले पशुत्व का यज्ञ करके कृत- कृत्य-सफल होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिए ।