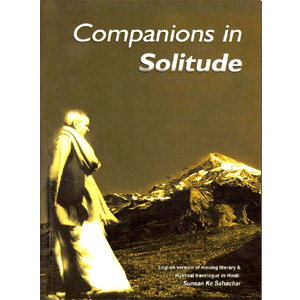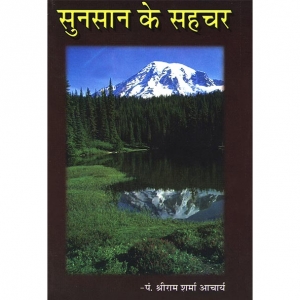सुनसान के सहचर 
हमारी जीवन साधना के अन्तरंग पक्ष-पहलू
Read Scan Versionहमारे बहुत से परिजन हमारी साधना और उसकी उपलब्धियों के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं और वह स्वाभाविक भी है। हमारे स्थूल जीवन के जितने अंश प्रकाश में आए हैं, वे लोगों की दृष्टि से अद्भुत हैं। उनमें सिद्धियों, चमत्कारों और अलौकिकताओं की झलक देखी जा सकती है। कौतूहल के पीछे उसके रहस्य को जानने की उत्सुकता स्वाभाविक है, सो अगर लोग हमारी आत्म- कथा जानना चाहते हैं, उसके लिए इन दिनों विशेष रूप से दबाव देते हैं। तो उसे अकारण नहीं कहा जा सकता।
यों हम कभी छिपाव के पक्ष में नहीं रहे- दुराव छल, कपट हमारी आदत में नहीं; पर इन दिनों हमारी विवशता है कि जब- तक रंग- मंच पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा अभिनय चल रहा है, तब तक वास्तविक को बता देने पर दर्शकों का आनंद दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा और जिस कर्तव्यनिष्ठा को सर्वसाधारण में जगाना चाहते हैं, वह प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। लोग रहस्यवाद के जंजाल में उलझ जायेंगे, इससे हमारा व्यक्तित्व भी विवादास्पद बन जाएगा और जो करने कराने हमें भेजा गया है उसमें भी अड़चन पड़ेगी। नि:संदेह हमारा जीवन अलौकिकताओं से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक हैं कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकर ही होगा। पीछे वालों के लिए उसे छोड़ देते हैं कि वस्तुस्थिति की सचाई को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसें और जितनी हर दृष्टि से परखी जाने पर सही निकले उससे यह अनुमान लगाएँ कि अध्यात्म विद्या कितनी समर्थ और सारगर्भित है। उस पारस से छूकर एक नगण्य- सा व्यक्ति अपने लोहे जैसे तुच्छ कलेवर को स्वर्ण जैसा बहुमूल्य बनाने में कैसे समर्थ, सफल हो सका। इस दृष्टि से हमारे जीवन- क्रम में प्रस्तुत हुए अनेक रहस्यमय तथ्यों की समय आने पर शोध की जा सकती है और उस समय उस कार्य में हमारे अति निकटवर्ती सहयोगी कुछ सहायता भी कर सकते हैं; पर अभी वह समय से पहले की बात है। इसलिए उस पर वैसे ही पर्दा रहना चाहिए, जैसे अब तक पड़ा रहा है।
आत्मकथा लिखने के आग्रह को केवल इस अंश तक पूरा कर सकते हैं कि हमारा साधना क्रम कैसे चला। वस्तुत: हमारी सारी उपलब्धियाँ प्रभु समर्पित साधनात्मक जीवन प्रक्रिया पर ही अवलम्बित है। उसे जान लेने से इस विषय में रूचि रखने वाले हर व्यक्ति को वह रास्ता मिल सकता है, जिस पर चल कर कि आत्मिक प्रगति और उससे जुड़ी विभूतियों का आनंद लिया जा सकता है। पाठकों को अभी इतनी ही जानकारी हमारी कलम से मिल सकेगी, सो उतने से ही इन दिनों सन्तोष करना पड़ेगा।
६० वर्ष के जीवन में से १५ वर्ष का आरम्भिक बाल जीवन कुछ विशेष महत्त्व का नहीं है। शेष पाँच वर्ष हमने आध्यात्मिकता के प्रसंगों को अपने जीवन- क्रम में सम्मिलित करके बिताये हैं, पूजा- उपासना का उस प्रयोग में बहुत छोटा अंश रहा है। २४ वर्ष तक ६ घंटे रोज की गायत्री उपासना को उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, जितना कि मानसिक और भावनात्मक उत्कृष्टता के अभिवर्धन के प्रयत्नों को। यह माना जाना चाहिए कि यदि विचारणा और कार्यपद्धति को परिष्कृत न किया गया होता, तो उपासना के कर्मकाण्ड उसी तरह निरर्थक चले जाते, जिस तरह कि अनेक पूजा- पत्री तक सीमित मन्त्र- तन्त्रों का ताना- बाना बुनते रहने वालों को नितान्त खाली रहना पड़ता है। हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए और उसमें दीखने वाली अलौकिकता को खोजा जाए तो उसका प्रधान कारण हमारी अन्तरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए। पूजा उपासना को गौण समझा जाए। आत्मकथा के एक अंश को लिखने का दुस्साहस करते हुए हम एक ही तथ्य का प्रतिपादन करेंगे कि हमारा सारा मनोयोग और पुरुषार्थ आत्म- शोधन में लगा है। उपासना जो बन पड़ी है, उसे भी हमने भाव परिष्कार के प्रयत्नों के साथ पूरी तरह जोड़ रखा है। अब आत्मोद्घाटन के साधनात्मक प्रकरण पर प्रकाश डालने वाली कुछ चर्चाएँ पाठकों की जानकारी के लिए करते हैं_
साधनात्मक जीवन की तीन सीढ़ियाँ हैं। तीनों पर चढ़ते हुए एक लंम्बी मंजिल पार कर ली गई। (१) मातृवत् परदारेषु (२) परद्रव्येषु लोष्ठवत् की मंजिल सरल थी, वह अपने- आप से सम्बन्धित थी। लड़ना अपने से था, संभालना अपने को था, तो पूर्व जन्मों के संस्कार और समर्थ गुरू की सहायता से इतना सब आसानी से बन गया। मन उतना ही दुराग्रही दुष्ट न था, जो कुमार्ग पर घसीटने की हिम्मत करता। यदा- कदा उसने इधर- उधर भटकने की कल्पना भर की। जब प्रतिरोध का डंडा जोर से सिर पर पड़ा ,, तो सहम गया और चुपचाप सही राह चलता रहा। मन से लड़ते, झगड़ते, पाप और पतन से भी बचा लिया गया। अब जबकि सभी खतरे टल गये तब संतोष की साँस ले सकते हैं। दास कबीर ने झीनी- झीनी बीनी चदरिया, जतन से ओढ़ी थी और बिना दाग- धब्बे ज्यों की त्यों वापिस कर दी। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि उसने सही राह पर हमें चला दिया और उन्हीं पदचिन्हों को ढ़ूढ़ते तलाशते, उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़े हुए उस स्थान तक पहुँच गये, जहाँ लुढ़कने और गिरने का खतरा नहीं रहता।
अध्यात्म की कर्मकाण्डात्मक प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती। संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा भी कम न पड़े तो मानसिक उव्दिग्नतानहीं होती और शांतिपूर्वक मन लगने लगता है। और उपासना के विधि- विधान गड़बड़ाए बिना अपने ढ़र्रे पर चलते रहते हैं। मामूली दुकानदार सारी जिन्दगी एक ही दुकान पर, एक ही ढर्रे से पूरी दिलचस्पी के साथ काट लेता है। न मन डूबता है न अरुचि होती है। पान- सिगरेट के दुकानदार १२- १४ घण्टे अपने धन्धे को उत्साह और शान्ति के साथ आजीवन करते रहते हैं, तो हमें ६- ७ घण्टे प्रतिदिन की गायत्री साधना २४ वर्ष तक चलाने का संकल्प तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती। मन उनका उचटता है जो उपासना को पान- बीड़ी की खेती- बाड़ी का, मिठाई- हलवाई के धन्धे से भी कम लाभदायक समझते हैं। बेकार के अरुचिकर कामों में मन नहीं लगता।
उपासना में ऊबने और अरूचि कि अड़चन उन्हें आती है जिनकी आन्तरिक आकांक्षा भौतिक सुख- सुविधाओं को सर्वस्व मानने की है, जो पूजा- पत्री से मनोकामनाएँ पूर्ण करने की बात सोचते रहते हैं उन्हें ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण अभिष्ठ वरदान न मिलने पर खीझ होती है। आरम्भ में ही आकांक्षा के प्रतिकूल काम में उदासी रहती है। यह स्थिति दूसरों की होती है, सो वे मन न लगने की शिकायत करते रहते हैं। अपना स्तर दूसरा था। शरीर बहाना- भर माना, वस्तुओं को निर्वाह की भट्ठी जलाने के लिए ईंधन भर समझा। महत्त्वाकाँक्षाएँ बड़ा आदमी बनने और झूठी वाह वाही लूटने की कभी नहीं उठी। जो यही सोचता रहा हम आत्मा हैं, तो क्यों न आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मशान्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए और आत्मविस्तार के लिए जिएँ। शरीर और अपने को जब दो भागों में बाँट दिया। शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग बाँट दिए तो तो अज्ञात की एक भारी दीवार अपने आप गिर पड़ी और अंधेरे से उजाला हो गया। उपासना में ऊबने और अरुचि की अड़चन उन्हें आती है जिनकी आन्तरिक आकांक्षा भौतिक सुख- सुविधाओं को सर्वस्व मानने की है, जो पूजा- पत्री को मनोकामनाएँ पूर्ण करने की बात सोचते रहते हैं उन्हें ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण अभिष्ट वरदान न मिलने पर खीझ होती है। आरम्भ में ही आकांक्षा के प्रतिकूल काम में उदासी रहती है। यह स्थिति दूसरों की होती है, सो वे मन न लगने की शिकायत करते रहते हैं। अपना स्तर दूसरा था। शरीर बहाना- भर माना, वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने का ईंधन भर समझा। महत्त्वाकांक्षाएँ बड़ा आदमी बनने और झूठी वाह वाही लूटने की कभी नहीं उठी। जो यही सोचता रहा हम आत्मा हैं, तो क्यों न आत्मोत्कर्ष के ली, आत्मशान्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए और आत्मविस्तार के लिए जिएँ। शरीर और अपने को जब दो भागों में बाँट दिया। शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग बाँट दिए तो वह अज्ञात की एक भारी दीवार अपने आप गिर पड़ी और अंधेरे से उजाला हो गया।
जो लोग अपने को शरीर मान बैठते हैं, इन्द्रिय तृप्ति तक अपना आनन्द सीमित कर लेते, वासना और तृष्णा कि पूर्ति ही जिनका जीवनोद्देश्य बन जाता है,उनके लिए पैसा, अमीरी, बड़प्पन,प्रशंसा, पदवी पाना ही सब कुछ हो सकता है। वे आत्म- कल्याण की बात भुला सकते हैं और लोभ- मोह की सुनहरी हथकड़ी- बेड़ी चावपूर्वक पहने रह सकते हैं। उनके लिए श्रेय पथ पर चलने की सुविधाजनक स्थिति न मिलने का बहाना सही हो सकता है। अंत:करण की आकांक्षाएँ ही साधन जुटाती हैं। जब भौतिक सुख सम्पत्ति ही लक्ष्य बन गया, तो चेतना का सारा प्रयास उन्हें जुटाने में लगेगा। उपासना तो फिर हल्की सी खिलवाड़ रह जाती है। कर ली तो ठीक, न कर ली तो ठीक। कौतूहल की दृष्टि से लोग देखा करते हैं कि लोग इनका थोड़ा तमाशा देख लें, कुछ मिलता है या नहीं- थोड़ी देर अनमनी तबियत से चमत्कार मिलने की दृष्टि से उल्टी- पुल्टी पूजा- पत्री चलाई तो उन पर विश्वास नहीं जमा, सो छूट गई, छूटनी भी थी। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में, जीवनोद्देश्य प्राप्त करने की तीव्र लगन के अभाव में कोई आत्मिक प्रगति नहीं कर सकता। यह सब तथ्य हमें अनायास ही विदित थे। सो शरीर यात्रा और परिवार व्यवस्था जमाये भर रहने के लिए जितना अनिवार्य रूप से आवश्यक था उतना ही ध्यान उस ओर दिया। उन प्रयत्नों को मशीन का किराया भर चुकाने की दृष्टि से किया। अन्त:करण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहा सो भौतिक प्रलोभनों और आकर्षणों में भटकने की कभी जरुरत नहीं हुई।
जब अपना स्वरूप आत्मा की स्थिति में होने लगा और अन्त:करण परमेश्वर का परम पवित्र निवास दीखने लगा तो चित्त अंतर्मुखी हो गया। सोचने का तरीका इतना भर सीमित रह गया कि परमात्मा के राजकुमार आत्मा को क्या करना, किस दिशा में चलना चाहिए? प्रश्न सरल थे और उत्तर भी सरल। केवल उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए और केवल आदर्शवादी कार्य- पद्धति अपनानी चाहिए। जो इस मार्ग पर चले नहीं, उन्हें बहुत डर लगता है कि यह रीति- नीति अपनाई तो बहुत संकट आवेगा और गरीबी, तंगी, भर्त्सना और कठिनाई सहनी पड़ेगी। मित्र शत्रु हो जायेंगे और घर वाले विरोध करेंगे, अपने को भी आरम्भ में ऐसा ही लगा और अनुभव हुआ। आरम्भिक दिनों मे हमें उपहास और भर्त्सना सहनी पड़ी। घर परिवार के लोग ही सबसे अधिक आड़े आये। उन्हें लगने लगा कि इसकी सहायता से जो भौतिक लाभ हमें मिलते हैं या मिलने वाले हैं उनमें कमी आ जायेगी, सो वे अपनी हानि जिसमें समझते, उसे भारी मूर्खता बताते थे, पर यह बात देर तक नहीं चली। अपनी आस्था ऊँची और सुदृढ़ हो, तो झूठ, विरोध देर तक नहीं टिकता, कुमार्ग पर चलने के कारण जो विरोध, तिरस्कार उत्पन्न होता है वही स्थिर रहता है। नेकी अपने आप में एक विभूति है, जो स्वयं का ही नहीं सभी का हित साधती है, इसीलिए स्थिर रहती भी है। विरोधी और निंदक कुछ ही दिनों में अपनी भूल समझ जाते हैं और रोड़ा अटकाने के बजाय सहयोग देने लगते हैं। आस्था जितनी ऊँची और जितनी मजबूत होगी, प्रतिकूलता उतनी ही जल्दी अनुकूलता में बदल जाती है। परिवार का विरोध देर तक नहीं सहना पड़ा, उनकी शंका- कुशंका वस्तु स्थिति समझ लेने पर दूर हो गई। आत्मिक जीवन में वस्तुत: घाटे की कोई बात नहीं है। बाहरी दृष्टि से गरीब दीखने वाला व्यक्ति आत्मिक दृष्टि शान्ति और सन्तोष के कारण बहुत प्रसन्न रहता है। यह प्रसन्नता और सन्तुष्टि हर किसी को प्रभावित करती है। जो विरोधियों को सहयोगी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। अपनी कठिनाई ऐसे ही हल हुई।
बड़प्पन का लोभ- मोह, वाहवाही की- तृष्णा की हथकड़ी- बेड़ी और तौक कटी तो लगा कि भव- बंधनों से मुक्ति मिल गयी। इन्हीं तीन जंजीरों में जकड़ा हुआ प्राणी इस भवसागर में औंधे मुँह घसीटा जाता रहता है और अतृप्ति, उद्विग्नता कि व्यथा वेदना से कराहता रहता है। इन तीनों की तुच्छता समझ ली जाय और लिप्सा को श्रद्धा में बदल दिया जाय, तो समझना चाहिए कि माया के बंधन टूट गए और जीवित रहते ही मुक्ति पाने का प्रयोजन पूरा हो गया। "नजरें तेरी बदलीं कि नजारा बदल गया" वाली उक्ति के अनुसार अपनी भावनाएँ, आत्मज्ञान होते ही समाप्त हो गईं और जीवन लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता अँगुली पकड़ कर मार्गदर्शन करने लगी, फिर अभाव रहा न असंतोष। शरीर को जीवित भर रखने और परिवार की, देह की परिस्थिति जितने साधनों से संतुष्ट रहने की शिक्षा देकर लोभ- लिप्सा की जड़ काट दी। मन उधर से भटकना बंद कर दे, तो कितनी अपार शक्ति मिलती है और जी कितना प्रफुल्लित रहता है। यह तथ्य कोई अनुभव करके देख सकता है; पर लोग तो ठहरे, तेल से आग बुझाना चाहते हैं। तृष्णा को दौलत से और वासना को भोग- साधना से तृप्त करना चाहते हैं। इन्हें कौन समझाये कि यह प्रयास केवल दावानल ही भड़का सकते हैं। इस पथ पर चलने वाला मृग- तृष्णा में ही भटक सकता है। मरघट के प्रेत- पिशाच की तरह उद्विग्न ही रह सकता है- कुकर्म ही कर सकता है। इसे कौन कैसे समझाये? समझने और समझाने वाले दोनों विडम्बना मात्र करते हैं। सत्संग और प्रवचन बहुत सुने, पर ऐसे ज्ञानी न मिले जो अध्यात्म के अन्तरंग में उतर कर अनुकरण की प्रेरणा देते। प्रवचन देने वाले के जीवनक्रम को उघाड़ा, तो वहाँ सुनने वाले से भी अधिक गन्दगी पाई। सो जी खट्टा हो गया।
बड़े- बड़े सत्संग, सम्मेलन होते तो, पर अपना जी किसी को देखने- सुनने के लिए न करता। प्रकाश मिला तो अपने भीतर। आत्मा ने ही हिम्मत की और चारों ओर जकड़े पड़े जंजाल को काटने की बहादुरी दिखाई, तो ही काम चला। दूसरों के सहारे बैठे रहते, तो ज्ञानी बनने वाले शायद अपने तरह हमें अज्ञानी बना देते। लगता है किसी को प्रकाश मिलना होगा, तो भीतर से ही मिलेगा। कम- से अपने सम्बन्ध में तो यही तथ्य सिद्ध हुआ है। आत्मिक प्रगति में वाह्य अवरोधों के जो पहाड़ खड़े थे- उन्हें लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखे बिना, श्रेय पथ पर चलने का दुस्साहस संग्रह किये बिना निरस्त नहीं किया जा सकता था, सो अपनी हिम्मत ही काम आई। अब अड़ गये तो सहायकों की भी कमी नहीं। गुरुदेव से लेकर भगवान् तक सभी अपनी मंजिल को सरल बनाने में सहायता देने के लिए निरन्तर आते रहे और प्रगति पथ पर धीरे- धीरे किन्तु सुदृढ़ कदम आगे ही बढ़ते चले गये। अब तक की मंजिल इसी क्रम से पूरी हुई है।
लोग कहते रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है; पर अपनी अनुभूति इससे सर्वथा विपरीत है। वासनाओं और तृष्णाओं से घिरा और भरा जीवन ही वस्तुत: कठिन एवं जटिल है। इस स्तर का क्रिया- कलाप अपनाने वाला व्यक्ति जितना श्रम करता है, जितना चिन्तित रहता है, जितनी व्यर्थ वेदना सहता है, जितना उलझा रहता है, उसे देखते हुए आध्यात्मिक जीवन की असुविधा को तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य ही कहा जा सकता है। इतना श्रम, इतना चिन्तन, इतना उद्वेग फिर भी क्षण भर भी चैन नहीं। कामना पूर्ति के लिए प्रथम प्रयास कर पूर्ति से पहले ही अभिलाषाओं का और सौ गुना हो जाना इतना बड़ा जंजाल है कि बड़ी- से सफलताएँ पाने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त और असंतुष्ट ही बना रहता है। छोटी सफलता पाने के लिए कितने थकान वाला श्रम करना पड़ा था, यह जानते हुए भी उससे बड़ी सफलता पाने के लिए चौगुने, दस गुने उत्तरदायित्व और ओढ़ लेता है। गति जितनी तीव्र होती जाती है उतनी ही समस्याएँ उठती और उलझती हैं। उन्हें सुलझाने में देह, मन और आत्मा का कचूमर निकलता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम सुरसा जैसी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता, अस्तु अनीति और अनाचार का मार्ग अपनाना पड़ता है। जघन्य पाप कर्म करते रहने पर अभिलाषाएँ पूर्ण नहीं होती हैं। निरन्तर की उव्दिग्नता और भविष्य की अंध तमिस्रा दोनों को मिलाकर जितनी क्षति है उसे देखते हुए उपलब्धियों को अति तुच्छ ही कहा जा सकता है।
आमतौर से लोग रोते- कलपते, रोग- शोक से सिसकते- बिलखते किसी प्रकार जिन्दगी की लाश ढोते हैं। वस्तुत: इन्हीं को तपस्वी कहा जाना चाहिए। कष्ट, त्याग, उद्वेग यदि आत्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए सहा जाता, तो मनुष्य योगी, सिद्ध पुरुष, महामानव, देवता ही नहीं भगवान् भी बन सकता था। बेचारों ने पाया कुछ नहीं, खोया बहुत। वस्तुत: यही सच्चे परोपकारी, आत्मदानी और बलिदानी हैं, जिन्होने परिश्रम से लेकर पाप की गठरी ढोने तक का दुस्साहस कर डाला और जो कमाया था उसे साले- बहनोई, बेटे- भतीजों के लिए छोड़कर स्वयं खाली हाथ चल दिए। दूसरे के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहने वाले वस्तुत: यही महात्मा, ज्ञानी, परमार्थी अपने को दीखते हैं। वे स्वयं अपने को मायाग्रस्त और पथभ्रष्ट कहते हैं तो कहते रहें
अपने इर्द- गिर्द घिरे असंख्यों मानव देहधारियों के अन्तरंग और बहिरंग जीवन की- उसकी प्रतिक्रिया परिणति को जब- हम देखते हैं,तो लगता है, इन सबसे सुख और सुविधा जनक जीवन हमीं ने जी लिया। हानि अधिक से अधिक इतनी हुई कि हमें कम सुविधा और सम्पन्नता का जीवन जीना पड़ा। सम्मान कम रहा और गरीब जैसे दीखे, सम्पदा न होने के कारण दुनियाँ वालों ने हमें छोटा समझा और अवहेलना की। बस इससे अधिक घाटा किसी आत्मवादी को नहीं हो सकता, पर इस अभाव से अपना कुछ भी हर्ज नहीं हुआ, न कुछ काम रुका। दूसरे षड़ष व्यंजन खाते रहे, हमने जौ- चना खाकर काम चलाया। दूसरे जीभ के अत्याचार से पीड़ित होकर रुग्णता का कष्ट सहते रहे, हमारा सस्ता आहार ठीक तरह पचता रहा और निरोगिता बनाये रहा। घाटे में हम क्या रहे? जीभ का क्षणिक जायका खोकर हमने "किवाड़- पापड़" होने की उक्ति सार्थक होती देखी। जहाँ तक जायके का प्रश्न है, उस दृष्टि से तुलना करने पर विलासियों की तुलना में हमारी जौ की रोटी अधिक मजेदार थी। धन के प्रयास में लगे लोग बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर, बढ़िया साज- सज्जा अपनाकर अपना अहंकार पूरा करने और लोगों पर रौब गाँठने की विडम्बना में लगे रहे। हम स्वल्प साधनों में उतना ठाठ तो जमा नहीं सके, पर सादगी ने जो आत्म- संतोष और आनन्द प्रदान किया उससे कम प्रसन्नता नहीं हुई, चाहे छिछोरे- बचकाने लोग मखौल उड़ाते रहे हों, पर वजनदार लोगों ने सादगी के पर्दे के पीछे झाँकती हुई महानता को सराहा और उसके आगे सिर झुकाया। नफे में कौन रहा, विडम्बना बनाने वाले या हम?
अपनी कसौटी पर अपने आपको कसने के बाद यही कहा जा सकता है कि कम परिश्रम, कम जोखिम और कम जिम्मेदारी लेकर हम शरीर, मन की दृष्टि से अधिक सुखी रहे और सम्मान भी कम नहीं पाया, पागल प्रशंसा न करें इसमें हमें एतराज नहीं- पर अपने आप से हमें कोई शिकायत नहीं- आत्मा से लेकर परमात्मा तक सज्जनों से लेकर दूरदर्शियों तक अपनी क्रिया पद्धति प्रशंसनीय मानी गयी। जोखिम भी कम और नफा भी ज्यादा।
खर्चीली, तृष्णाग्रस्त, बनावटी, भारभूत जिन्दगी पाप और पतन के पहियों वाली गाड़ी पर ढोई जा सकती है। अपना सबकुछ हल्का रहा, बिस्तर बगल में दबाया और चल दिये। न थकान, न चिन्ता, हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि आदर्शवादी जीवन सरल है। उसमें प्रकाश, सन्तोष, उल्लास सबकुछ है। दुष्ट लोग आक्रमण करके कुछ हानि पहुँचा दें, तो यह जोखिम पापी और घृणित जीवन में भी कम कहाँ है? सन्त और सेवाभावियों को जब इतना त्रास सहना पड़ता है, तो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या- व्देष और प्रतिशोध के कारण भौतिक जीवन में और भी अधिक खतरा रहता है। कत्ल, खून, डकैती, आक्रमण की जो रोमांचकारी घटनाएँ जो आये दिन सुनने को मिलती रहती हैं उनमें भौतिक जीवन जीने वाले ही अधिक मरते- खपते देखे जाते हैं। इतने व्यक्ति अगर स्वेच्छापूर्वक अपने प्राण और धन गँवाने को मजबूर हो जाते, तो उन्हें देवता माना जाता और इतिहास धन्य हो जाता।
ईसा, सुकरात, गाँधी जैसे सन्त या उस वर्ग के लोग थोड़ी संख्या में ही मरे हैं। उससे हजार गुने अधिक की तो पतन्मुखी क्षेत्र में ही हत्याएँ होती रहती हैं। दान से गरीब हुए भामाशाह तो उँगलियों पर गिने जाने वाले ही मिलेंगे पर ठगी, विश्वासघात, व्यसन, व्यभिचार, आक्रमण, मुकदमा, बीमारी, बेवकूफी के शिकार होने वाले आये दिन अमीर के फकीर बनते लाखों व्यक्ति रोज ही देखे जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में घाटा, आक्रमण, मुकदमा, कम है, भौतिक में अधिक। इस तथ्य को अगर ठीक तरह से समझा गया होता, तो लोग आदर्शवादी जीवन से घबराने और भौतिक लिप्सा में औंधे मुँह गिरने की बेवकूफी न करते। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि तृष्णा- वासना के प्रलोभन में व्यक्ति पाता कम खोता अधिक है। हमें जो खोना पड़ा वह नगण्य है, जो पाया वह इतना अधिक है कि जी बार- बार यही सोचता है कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने को उत्कृष्ट और आदर्शवादी परम्परा अपनाने के लिए कहा जाय्, पर बात मुश्किल है। हमें अपने अनुभवों को साक्षी देकर उज्ज्वल जीवन जीने की गुहार मचाते मुद्दत हो गयी, पर कितनों ने उसे सुना और सुनने वालों में से कितनों ने उसे अपनाया?
मातृवत् परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत् की दो सीढ़ियाँ चढ़ना भी अपने को कठिन पड़ता, यदि जीवन का स्वरूप, प्रयोजन और उपयोग ठीक तरह से समझाने और जो श्रेयस्कर है उसी पर चलने की हिम्मत और बहादुरी नहीं होती। जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा और तृष्णा- वासना के लिए आतुर रहा उसे आत्मिक प्रगति से वंचित रहना पड़ा है। पूजा, उपासना के छिटपुट कर्मकाण्डों के बल पर प्रगति की नाव किनारे नहीं लगी है। हमें २४ वर्ष तक निरंतर गायत्री पुरश्चरणों में निरत रह कर उपासना का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय पूरा करना पड़ा। उस पर कर्मकाण्ड की सफलता का पूरा लाभ तभी संभव हो सका जब अत्यधिक प्रगति की भावनात्मक प्रक्रिया को, जीवन- साधना को उससे जोड़े रखा। यदि दूसरों की तरह हम देवताओं को वश में करने या ठगने के लिए, उनसे मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए तन्त्र- मन्त्र का कर्मकाण्ड रचते रहते- जीवन क्रम निर्वाह की आवश्यकता न समझते तो नि:संदेह हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ता। हम अगणित भजनानन्दी और तन्त्र- मन्त्र के कर्मकाण्ड़ियों को जानते हैं, जो अपनी धुन में मुद्दतों से लगे हैं। पूजा- पाठ हमसे ज्यादा लम्बा और चौड़ा है, पर बारीकी से जब उन्हें परखा तो छूँछ मात्र पाया, झूठी आत्म- प्रवंचना उनमें जरूर पायी, जिसके आधार पर यह सोचते थे कि इस जन्म में न सही- मरने के बाद उन्हें स्वर्ग- सुख जरूर मिलेगा; पर हमारी परख और भविष्यवाणी यह है कि इनमें से एक को भी स्वर्ग आदि मिलने वाला नहीं, न उन्हें कोई सिद्ध चमत्कार हाथ लगने वाला है।
कर्मकाण्ड और पूजा- पाठ में प्राण तभी आते हैं जब साधक का जीवन क्रम उत्कृष्टता की दिशा में क्रमबद्ध रीति से अग्रसर हो रहा हो। उसका दृष्टिकोण सुधर रहा हो और क्रिया कलाप में उस रीति- नीति का समावेश हो जो आत्मवादी के साथ आवश्यक रूप से जुड़े रहते हैं। धूर्त, स्वार्थी, कंजूस और सदा बेटी, बेटों के लिए जीने वाले लोग यदि अपनी विचारणा और गतिविधियाँ परिष्कृत न करें, तो उन्हें तीर्थ, व्रत, उपवास, कथा, कीर्तन, स्नान, ध्यान आदि का कुछ लाभ मिल सकेगा, इसमें हमारी सहमति नहीं है। यह उपयोगी तो हैं, पर इसकी उपयोगिता इतनी है जितनी कि लेख लिखने के लिए कलम की। कलम के बिना लेख कैसे लिखा जा सकता है? पूजा उपासना के बिना आत्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। यह जानने के साथ- साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि स्वास्थ्य, अध्ययन, चिन्तन, मनन की, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया सम्पन्न किये बिना केवल कलम कागज के आधार पर लेख नहीं लिखा जा सकता। न कविताएँ बनाई जा सकती हैं। आन्तरिक उत्कृष्टता बौद्धिक विकास की तरह है और पूजा अच्छी कलम की तरह। दोनों का समन्वय होने से ही बात बनती है। एक को हटा दिया जाय तो बात अधूरी रह जाती है। हमने यह ध्यान रखा कि साधना की गाड़ी एक पहिए पर न चल सकेगी, इसलिए दोनों पहियों की व्यवस्था ठीक तरह जुटाई जाय। हमने उपासना कैसे कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। गायत्री महाविज्ञान में जैसा लिखा है उसी क्रम से हमारा गायत्री मन्त्र का सामान्य उपासन क्रम चलता रहा है। हाँ! जितनी देर तक भजन करने बैठे हैं, उतनी देर तक यह भावना अवश्य करते रहे हैं ब्रह्म की परम तेजोमयी सत्ता माता गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे रोम- रोम में ओत- प्रोत हो रहा है और प्रचण्ड अग्नि में पड़कर लाल हुए लोहे की तरह हमारा भौंड़ा अस्तित्व उसी स्तर का उत्कृष्ट बन गया है जिस स्तर का कि हमारा इष्टदेव है। शरीर के अणु- परमाणुओं में गायत्री माता का वर्चस्व समा जाने से काया का हर अवयव ज्योर्तिमय हो उठा अग्नि से इन्द्रियों की लिप्सा जल कर भस्म हो गयी, आलस्य आदि दुर्गुण नष्ट हो गये। रोग- विकारों को उस अग्नि ने अपने में जला दिया।
शरीर तो अपना है, पर उसके भीतर प्रचंड ब्रह्मवर्चस लहरा रहा है, व वाणी में केवल सरस्वती ही शेष है। असत्य, छल और स्वाद के वह असुर उस दिव्य मंदिर को छोड़कर पलायन कर गये। नेत्रों में गुण ग्राहकता और भगवान् का सौन्दर्य हर जड़- चेतन में देखने की क्षमता भर शेष है। छिद्रान्वेषण, कामुकता जैसे दोष आँखों में नहीं रहे। कान केवल जो मंगलमय हैं उसे सुनते हैं। बाकी कोलाहल मात्र है जो श्रवणेन्द्रिय के पर्दे से टकरा कर वापस लौट जाता है।
गायत्री माता का परम तेजस्वी प्रकाश सूक्ष्म शरीर में- अंत:करण में- मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रवेश करते और प्रकाशवान होते देखा तथा अनुभव किया कि ब्रह्मवर्चस अपने मन को उस भूमिका में घसीटे लिए जा रहा है जिसमें पाशविक इच्छा आकाँक्षाएँ विरत हो जाती हैं और दिव्यता परिप्लावित करने वाली आकांक्षाएँ सजग हो उठती हैं। बुद्धि निर्णय करती है कि क्षणिक आवेशों के लिए, तुच्छ प्रलोभनों के लिए मानव जीवन जैसी उपलब्धि विनष्ट नहीं की जा सकती। इसका एक- एक पल आदर्शों की प्रतिष्ठापना के लिए खर्च किया जाना चाहिए। चित्त में उच्च निष्ठाएँ जमानी और सत्यम्- शिवम् कि ओर बढ़ चलने की उमंगें उत्पन्न करनी हैं। सविता देवता का तेजस अपनी अन्त:भूमिका में प्रवेश करके "अहं'' को परिष्कृत करता है। मरणधर्मा जीवधारियों की स्थिति से योजनों ऊपर उड़ा ले जाकर ईश्वर के सर्व समर्थ, परम पवित्र और सच्चिदानन्द स्वरूप में अवस्थित कर देता है।
गायत्री पुरश्चरणों के समय केवल जप ही नहीं किया जाता रहा, साथ ही भाव तरंगों से मन भी हिलोरें लेता रहा। कारण शरीर भावभूमि का अन्त:स्थल के आत्मबोध, आत्म दर्शन, आत्मानुभूति और आत्म विस्तार की अनुभूति अन्तर्ज्योति के रूप में अनुभव किया जाता रहा। लगा अपनी आत्मा परम तेजस्वी सविता देवता के प्रकाश में पतंगों के दीपक पर समर्पित होने की तरह विलीन हो गयी। अपना अस्तित्व समाप्त, उसकी स्थान पूर्ति परम तेजस् व्दारा। मैं समाप्त- सत् का आधिपत्य्। आत्मा और परमात्मा के अव्दैत मिलने की अनुभूति में ऐसे ब्रह्मानन्द की सरसता की क्षण- क्षण अनुभूति होती रही जिस पर संसार भर का समवेत विषयानन्द निछावर किया जा सकता है। जप के साथ स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरों में दिव्य प्रकाश की प्रतिष्ठापना का आरम्भ प्रयत्न पूर्वक धारण के रूप में की गई थी। पीछे वह स्वाभाविक प्रकृति बनी और अन्तत: प्रत्यक्ष अनुभूति बन गई। जितनी देर उपासना में बैठा गया- अपनी सत्ता के भीतर और बाहर परम तेजस्वी सविता की दिव्य ज्योति का सागर लहलहाता रहा और यही प्रतीत होता रहा कि हमारा अस्तित्व इस दिव्य ज्योति से ओतप्रोत हो रहा है। प्रकाश के अतिरिक्त अंतरंग और बहिरंग में और कुछ है ही नहीं। प्राण के हर स्फुरण में ज्योति स्फुल्लिंगों के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। इस अनुभूति ने कम से कम पूजा के समय की अनुभूति को दिव्य दर्शन अनुभव से ओतप्रोत बनाए ही रखा। साधना का प्राय: सारा समय इसी अनुभूति के साथ बीता।
पूजा के ६ घंटे, शेष और १८ घण्टों की भरपूर प्रेरणा देते। काम का जो समय रहा उसमें यह लगता रहा कि इष्ट देवता का तेजस् ही अपना मार्गदर्शक है। उनके संकेतों पर ही प्रत्येक क्रिया- कलाप बना और चल रहा है। लालसा और लिप्सा से, तृष्णा और वासना से प्रेरित अपना कोई कार्य हो रहा हो ऐसा कभी लगा ही नहीं। छोटे बालक को माँ जिस तरह उँगली पकड़कर चलाती है, उसी प्रकार दिव्य सत्ता ने मस्तिष्क को पकड़कर ऊँचा सोचने और शरीर को पकड़कर ऊँचा करने के लिए विवश कर दिया। उपासना के अतिरिक्त जाग्रत अवस्था के जितने घण्टे रहे उनमें शारीरिक नित्य कर्मों से लेकर आजीविका, उपार्जन, स्वाध्याय- चिन्तन परिवार व्यवस्था आदि की समस्त क्रियाएँ इस अनुभूति के साथ चलती रहीं मानो परमेश्वर इन सबका नियोजन और संचालन कर रहा हो। रात को सोने के ६ घण्टे ऐसी गहरी नींद में बीतते रहे मानों समाधि लग गई हो और माता के आँचल में अपने को सौंप कर परम शान्ति और सन्तुष्टि की भूमिका आत्मसत्ता से तादात्म्य प्राप्त कर रही हो। सोकर जब उठे तो लगा- नया जीवन, नया उल्लास, नया प्रकाश अग्रिम मार्गदर्शन के लिए पहले से ही पथ प्रदर्शन के लिए पहले से ही पथ प्रदर्शन के लिए सामने खड़ा है।
२४ वर्ष के २४ महापुरश्चरण काल में कोई सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कन्धे पर नहीं थीं, सो अधिक तत्परता और तन्मयता के साथ यह जप- ध्यान का क्रम ठीक तरह चलता रहा। मातृवत् परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्ठवत् की अटूट निष्ठा ने काया को पाप कर्मों से बचाये रखा, अन्न की सात्विकता ने मन को अध:पतन के गर्त में गिरने से भली प्रकार रोक रखने में सफलता पाई। जौ की रोटी गाय की छाछ का आहार रुचा भी और पचा भी। जैसा अन्न वैसा मन की सचाई हमने अपने जीवन काल में पग- पग पर अनुभव की, यदि शरीर और मन का संयम कठोरतापूर्वक न बरता गया होता तो शायद जो थोड़ी सी प्रगति हो सकी, वह हो सकी होती या नहीं।