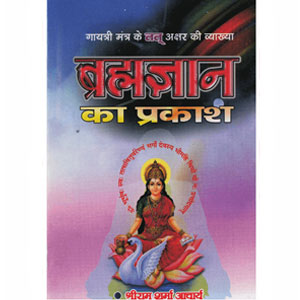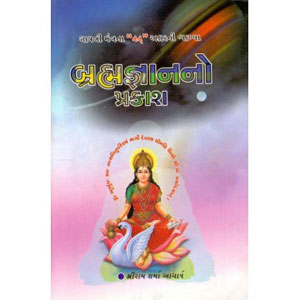ब्रह्मज्ञान का प्रकाश 
अपनी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाइए
Read Scan Version
समस्त आध्यात्मिक उपदेशों का सारांश यही निकलता है कि हमारी प्रवृत्ति बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होनी चाहिए । चेतना का प्रकाश जिस ओर जाता है उसी ओर आलोक हो जाता है और जिस ओर उसका प्रकाश नहीं जाता उस ओर अंधकार हो जाता है । चेतना के प्रकाश में दो विशेषताएँ हैं- एक वह पदार्थ का ज्ञान कराता है और दूसरे, वह उसे प्रिय बनाता है । उससे जिस ओर हमारी चेतना जाती है अर्थात जिन वस्तुओं की ओर हम ध्यान देते हैं, वे न केवल हमें ज्ञात हो जाती हैं वरन वे हमें प्रिय हो जाती हैं । जिन बातों के बारे में हम कुछ जानते नहीं, वे हमें प्रिय भी नहीं होतीं । मनुष्य को जो वस्तु प्यारी लगती है, वह उसकी वृद्धि करने की भी चेष्टा करता है । इस प्रकार चेतना से प्रकाशित वस्तुओं की वृद्धि इसी प्रकार होती है । शरीर की उन्नति भी शरीर के विषय में सोचने से होती है ।
जब मनुष्य बहिर्मुखी रहता है तो वह सांसारिक उन्नति करता है । उसके धन, यश और मान-प्रतिष्ठा बढ़ते हैं, पर उसका स्वत्व अंधकार में रह जाता है । अंधकार में रहने के कारण न तो मनुष्य को अपने आपका कुछ ज्ञान होता है और न उसे अपने आप प्रिय ही लगता है । इतना ही नहीं, बहिर्मुखी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप से इतना विफल हो जाएगा कि आत्महत्या करने की इच्छा होने लगेगी । यदि किसी कारण से बहिर्मुखी व्यक्ति को कभी अकेले रह जाना पड़ता है तो वे जीवन से निराश हो जाते हैं । उनके विचार उनके नियंत्रण में नहीं रहते । उनकी मानसिक ग्रंथियाँ उन्हें भारी त्रास देने लगती है और उन्हें जीवन भार रूप हो जाता है ।
चेतना का प्रकाश बाहर जाने से मनुष्य के मन में अनेकों प्रकार के संस्कार पड़ते हैं । ये सभी संस्कार मानसिक क्लेश के कारण बन जाते हैं । इनसे आत्मा की प्रियता कम हो जाती है और बाहरी पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ जाता है । इस प्रकार मनुष्य की चेतना के पीछे सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं के रूप में एक अचेतन मन की सृष्टि होती है । जो व्यक्ति जितना ही बहिर्मुखी हैं, उसकी सांसारिक पदार्थों की इच्छाएँ उतनी ही प्रबल होती हैं । इन ग्रंथियों के कारण मनुष्य का आंतरिक स्वत्व दुखी हो जाता है । वह फिर चेतना के प्रकाश को अपने आप के पास बुलाने का उपाय रचता है । रोग की उत्पत्ति अपने आप की ओर चेतना के प्रकाश के बुलाने का उपाय है ।
मनुष्य का वैयक्तिक अचेतन मन उसकी मानसिक ग्रंथियों और दलित इच्छाओं का बना हुआ है । दबी हुई इच्छाओं का चेतना पर प्रकाशित होने से रेचन हो जाता है और बहुत सी मानसिक ग्रंथियाँ इस प्रकार खुल जाती हैं, पर इससे मानसिक ग्रंथियों का बनना रुकता तक नहीं । नई मानसिक ग्रंथियाँ बनती ही जाती हैं । इस प्रकार अचेतन मन का नया भार तैयार होता जाता है । मनोविश्लेषण चिकित्सा से मनुष्य की व्याधि विशेष का उपचार हो जाता है पर उससे मूल रोग नष्ट नहीं होता ।
जब मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है तो बाह्य पदार्थों की प्रियता चली जाती है । उसके कारण वे मनुष्य के मन पर अपने दृढ़ संस्कार नहीं छोड़ते । इस प्रकार नया कर्म विपाक बनना बंद हो जाता है । सदा आध्यात्मिक चिंतन करने से मनुष्य की पुरानी मानसिक ग्रंथियाँ खुल जाती हैं । अब उसे अपने सुख के लिए इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ता । उसे अपने विचारों में असीम आनंद मिलने लगता है । अब अनेक प्रकार की सांसारिक चिंताएँ किसी प्रकार की मानसिक अशांति उत्पन्न नहीं करतीं । मनुष्य निजानंद में निमग्न रहता है । ऐसा व्यक्ति सदा साम्यावस्था में रहता है ।
चेतना का प्रकाश धीरे-धीरे भीतर की ओर मोड़ा जाता है । इसके लिए नित्य अभ्यास और विचार की आवश्यकता है । जब मनुष्य को बाह्य विषयों से विरक्ति हो जाती है अर्थात जब वे उसे दुःख रूप प्रतीत होने लगते हैं तभी वह सुख को अपने भीतर खोजने की चेष्टा करता है । मन के हताश होने की अवस्था में मनुष्य के विचार स्थिर नहीं रहते, वह सभी प्रकार के प्रयत्नों को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है । अतएव एकाएक मन को अंतर्मुखी नहीं बनाया जा सकता पर धीरे-धीरे उसे अभ्यास के द्वारा अंतर्मुखी बनाया जा सकता है ।
जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है तो उसे ज्ञात होता है कि मनुष्य का मानसिक संसार उसके बाह्य संसार के फैलाव से कम नहीं है । जितना बाह्य संसार का विस्तार है, उससे कहीं अधिक आंतरिक संसार का है अर्थात मनुष्य को आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक अध्ययन, विचार और अन्वेषण करना पड़ता है, जितना कोई भौतिक विज्ञान में रुचि रखने वाला अन्वेषक करता है ।
संसार की सभी वस्तुएँ आत्मसंतोष के लिए हैं । यदि मनुष्य को आत्म- संतोष का सरल मार्ग ज्ञात हो जाए तो वह सांसारिक पदार्थों के पीछे क्यों दौड़े ? पर यह आत्मसंतोष प्राप्त करना सरल काम नहीं है जितनी कठिनाई किसी इच्छित बाह्य पदार्थ के प्राप्त करने में होती है, उससे कहीं अधिक कठिनाई आत्मज्ञान प्राप्त करने में होती है । आत्मज्ञान मन की साधना से उत्पन्न होता है । जब तक मन निरवलंब नहीं हो जाता, तब तक निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, पर मन का सहज स्वभाव है आत्मा से इतर वस्तु पर अवलंबित होकर रहना । उसे अपनी इस आदत से मुक्त करने में जितना प्रयास करना पड़ता है, वह कल्पनातीत है ।
ईश्वरवाद में विश्वास रखने और उसके ध्यान में तल्लीन होने का मुख्य उद्देश्य यही कि आत्मा अपने वास्तविक सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को समझकर स्वावलंबी बन सके । ईश्वर की उपासना के द्वारा हम 'दिव्य सत् तत्त्व' की आराधना करते हैं, जिससे हमारी आत्मा तमोगुण और रजोगुण से छूटकर सत् तत्त्व में सरावोर हो जाए । नाना विधि-विधानों से, अनेकानेक कर्मकांडों से संसार भर में ईश्वर की जो पूजा-उपासना होती हुई दिखलाई पड़ती है, उस सब का मर्म यही है कि जीव ईश्वरीय सत्-तत्त्व के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाए और अंत में स्वयं भी वैसा ही बन जाए । उस अवस्था को प्राप्त हो जाने से आनंद की सीमा नहीं रहती । अनंत आनंद में उसकी चेतन तल्लीन हो जाती है । सत्त्वगुण की इसी परिपूर्णता को ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं ।
जब मनुष्य बहिर्मुखी रहता है तो वह सांसारिक उन्नति करता है । उसके धन, यश और मान-प्रतिष्ठा बढ़ते हैं, पर उसका स्वत्व अंधकार में रह जाता है । अंधकार में रहने के कारण न तो मनुष्य को अपने आपका कुछ ज्ञान होता है और न उसे अपने आप प्रिय ही लगता है । इतना ही नहीं, बहिर्मुखी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप से इतना विफल हो जाएगा कि आत्महत्या करने की इच्छा होने लगेगी । यदि किसी कारण से बहिर्मुखी व्यक्ति को कभी अकेले रह जाना पड़ता है तो वे जीवन से निराश हो जाते हैं । उनके विचार उनके नियंत्रण में नहीं रहते । उनकी मानसिक ग्रंथियाँ उन्हें भारी त्रास देने लगती है और उन्हें जीवन भार रूप हो जाता है ।
चेतना का प्रकाश बाहर जाने से मनुष्य के मन में अनेकों प्रकार के संस्कार पड़ते हैं । ये सभी संस्कार मानसिक क्लेश के कारण बन जाते हैं । इनसे आत्मा की प्रियता कम हो जाती है और बाहरी पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ जाता है । इस प्रकार मनुष्य की चेतना के पीछे सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं के रूप में एक अचेतन मन की सृष्टि होती है । जो व्यक्ति जितना ही बहिर्मुखी हैं, उसकी सांसारिक पदार्थों की इच्छाएँ उतनी ही प्रबल होती हैं । इन ग्रंथियों के कारण मनुष्य का आंतरिक स्वत्व दुखी हो जाता है । वह फिर चेतना के प्रकाश को अपने आप के पास बुलाने का उपाय रचता है । रोग की उत्पत्ति अपने आप की ओर चेतना के प्रकाश के बुलाने का उपाय है ।
मनुष्य का वैयक्तिक अचेतन मन उसकी मानसिक ग्रंथियों और दलित इच्छाओं का बना हुआ है । दबी हुई इच्छाओं का चेतना पर प्रकाशित होने से रेचन हो जाता है और बहुत सी मानसिक ग्रंथियाँ इस प्रकार खुल जाती हैं, पर इससे मानसिक ग्रंथियों का बनना रुकता तक नहीं । नई मानसिक ग्रंथियाँ बनती ही जाती हैं । इस प्रकार अचेतन मन का नया भार तैयार होता जाता है । मनोविश्लेषण चिकित्सा से मनुष्य की व्याधि विशेष का उपचार हो जाता है पर उससे मूल रोग नष्ट नहीं होता ।
जब मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है तो बाह्य पदार्थों की प्रियता चली जाती है । उसके कारण वे मनुष्य के मन पर अपने दृढ़ संस्कार नहीं छोड़ते । इस प्रकार नया कर्म विपाक बनना बंद हो जाता है । सदा आध्यात्मिक चिंतन करने से मनुष्य की पुरानी मानसिक ग्रंथियाँ खुल जाती हैं । अब उसे अपने सुख के लिए इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ता । उसे अपने विचारों में असीम आनंद मिलने लगता है । अब अनेक प्रकार की सांसारिक चिंताएँ किसी प्रकार की मानसिक अशांति उत्पन्न नहीं करतीं । मनुष्य निजानंद में निमग्न रहता है । ऐसा व्यक्ति सदा साम्यावस्था में रहता है ।
चेतना का प्रकाश धीरे-धीरे भीतर की ओर मोड़ा जाता है । इसके लिए नित्य अभ्यास और विचार की आवश्यकता है । जब मनुष्य को बाह्य विषयों से विरक्ति हो जाती है अर्थात जब वे उसे दुःख रूप प्रतीत होने लगते हैं तभी वह सुख को अपने भीतर खोजने की चेष्टा करता है । मन के हताश होने की अवस्था में मनुष्य के विचार स्थिर नहीं रहते, वह सभी प्रकार के प्रयत्नों को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है । अतएव एकाएक मन को अंतर्मुखी नहीं बनाया जा सकता पर धीरे-धीरे उसे अभ्यास के द्वारा अंतर्मुखी बनाया जा सकता है ।
जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है तो उसे ज्ञात होता है कि मनुष्य का मानसिक संसार उसके बाह्य संसार के फैलाव से कम नहीं है । जितना बाह्य संसार का विस्तार है, उससे कहीं अधिक आंतरिक संसार का है अर्थात मनुष्य को आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक अध्ययन, विचार और अन्वेषण करना पड़ता है, जितना कोई भौतिक विज्ञान में रुचि रखने वाला अन्वेषक करता है ।
संसार की सभी वस्तुएँ आत्मसंतोष के लिए हैं । यदि मनुष्य को आत्म- संतोष का सरल मार्ग ज्ञात हो जाए तो वह सांसारिक पदार्थों के पीछे क्यों दौड़े ? पर यह आत्मसंतोष प्राप्त करना सरल काम नहीं है जितनी कठिनाई किसी इच्छित बाह्य पदार्थ के प्राप्त करने में होती है, उससे कहीं अधिक कठिनाई आत्मज्ञान प्राप्त करने में होती है । आत्मज्ञान मन की साधना से उत्पन्न होता है । जब तक मन निरवलंब नहीं हो जाता, तब तक निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, पर मन का सहज स्वभाव है आत्मा से इतर वस्तु पर अवलंबित होकर रहना । उसे अपनी इस आदत से मुक्त करने में जितना प्रयास करना पड़ता है, वह कल्पनातीत है ।
ईश्वरवाद में विश्वास रखने और उसके ध्यान में तल्लीन होने का मुख्य उद्देश्य यही कि आत्मा अपने वास्तविक सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को समझकर स्वावलंबी बन सके । ईश्वर की उपासना के द्वारा हम 'दिव्य सत् तत्त्व' की आराधना करते हैं, जिससे हमारी आत्मा तमोगुण और रजोगुण से छूटकर सत् तत्त्व में सरावोर हो जाए । नाना विधि-विधानों से, अनेकानेक कर्मकांडों से संसार भर में ईश्वर की जो पूजा-उपासना होती हुई दिखलाई पड़ती है, उस सब का मर्म यही है कि जीव ईश्वरीय सत्-तत्त्व के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाए और अंत में स्वयं भी वैसा ही बन जाए । उस अवस्था को प्राप्त हो जाने से आनंद की सीमा नहीं रहती । अनंत आनंद में उसकी चेतन तल्लीन हो जाती है । सत्त्वगुण की इसी परिपूर्णता को ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं ।