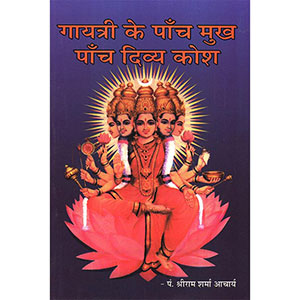गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश 
अन्नमय कोश का परिष्कार और प्रतिफल
Read Scan Version
भारतीय दर्शन के अन्तर्गत जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अन्नमय कोश की शुद्धि-पुष्टि और विकास को भी पर्याप्त महत्व दिया गया। भौतिकी प्रगति हो या आध्यात्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति—दोनों के लिये ही उसे आवश्यक और उपयोगी ठहराया गया है। योग साधनाओं में अन्नमय कोश की साधना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसके अनेक लाभों एवं सिद्धियों का भी उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा ही योगी आरोग्य तथा शरीर संस्थान पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इच्छानुसार शीरी को गर्म या ठण्डा रखना, ऋतुओं के प्रभाव से अप्रभावित रहना, शरीर की ऊर्जा पूर्ति के लिये आहार पर आश्रित न रहकर उसे सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर लेना, दीर्घ-जीवन, शरीर में वृद्धावस्था के चिन्ह न उभरना आदि सभी उपलब्धियां अन्नमय कोश की साधना पर निर्भर करती हैं।
यह सब उपलब्धियां आध्यात्मिक साधना मार्ग पर बढ़ने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है और सांसारिक जीवनक्रम में भी इनका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यह उपलब्धियां बड़ी आकर्षक भी लगती हैं। किन्तु योग मार्ग की यह बहुत प्रारम्भिक सीढ़ियां हैं। यह इसलिये आवश्यक है कि योग साधना के लिये आवश्यक साधनाक्रम में यह शरीर अपनी असमर्थता प्रकट करके साथ देने से कतराने न लगे। अन्नमय कोश शुद्ध और पुष्ट होने पर ही व्यक्ति सांसारिक उतार-चढ़ावों के बीच अपनी शरीर यात्रा को सन्तुलित क्रम से चलाता हुआ, अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर अनवरत क्रम से बढ़ सकता है।
एक और सूक्ष्म पक्ष है जिसके लिये अन्नमय कोश को तैयार करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति के क्रम में शरीर में अनेक दिव्य संवेदनाओं का संसार होता है। असंस्कारित अन्नमय कोश उसमें बाधक बन जाता है। अथवा वांछित सहयोग नहीं देने पाता। इस क्रम में अनेक दिव्य क्षमताएं उभरती हैं, उन्हें धारण करना उनके स्पन्दनों को सहन करके अपना सन्तुलन बनाये रखना भी बहुत आवश्यक है। यह सभी बातें परिष्कृत एवं विकसित क्षमता सम्पन्न अन्नमय कोश से ही सम्भव हैं।
इन सब उपलब्धियों एवं क्षमताओं का लाभ पाने के लिये अन्नमय कोश, उसके स्वरूप तथा सामान्य गुण धर्मों के बारे में भी साधक के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप रेखा होनी चाहिये। पांचों कोशों की संगति में अन्नमय कोश की भूमिका तथा उसके महत्व को उचित अनुपात में समझना आवश्यक है।
हमारी सत्ता, स्थूल-सूक्ष्म अनेक स्तर के तत्वों के संयोग से बनी है। उनमें से हर एक घटक का अपना-अपना महत्व है। किसी एक घटक का महत्व बतलाने से किसी दूसरे घटक का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे का सहयोगी पूरक तो है, किन्तु उसका स्थान वह स्वयं नहीं ले सकता। उदाहरण के लिये भवन निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट का गारा (मार्टर) लें। उसमें सीमेंट, बालू, पानी, रंग आदि सभी मिलाये जाते हैं। किसी एक का भी स्तर घटिया हो तो गारा घटिया हो जायेगा। उसकी लोच, मजबूती, सुन्दरता आदि इन सभी के सन्तुलित संयोग से है। हमारे अस्तित्व के बारे में भी यही तथ्य लागू होता है। हमारे अस्तित्व के हर घटक का, हर कोश का अपना-अपना महत्व है। इसीलिये उन सबकी उत्कृष्टता एवं सन्तुलन का ध्यान रखना आवश्यक है।
हमारी संरचना में एक बड़ा भाग वह है जिसका सीधा सम्बन्ध स्थूल पदार्थों—पंच भूतों से है। उसके अस्तित्व, पोषण एवं विकास के लिये स्थूल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर संस्थान के इसी भाग को अन्नमय कोश कहते हैं। यह अगणित छोटी-छोटी स्थूल इकाईयों से बना हुआ है। इन्हें कोशिका (सैल) कहते हैं। स्पष्ट है कि यह इकाइयां जिस प्रकार की, जिन गुण धर्मों से युक्त होगी, संयुक्त शरीर संस्थान में भी वही गुण धर्म प्रकट होंगे। उन मूल इकाइयों को बदले बिना बाह्य दृश्य संस्थान में इच्छित विशेषताएं पैदा नहीं की जा सकतीं। अन्नमय कोश को आवश्यकता के अनुरूप बनाने ढालने के लिये भी उसकी मूल इकाइयों को ध्यान में रखना होगा।
उदाहरण के लिये कोई वस्त्र लें। वस्त्र किस कोटि का है, यह इस आधार पर निर्भर करता है उसकी रचना में किस प्रकार के धागों का उपयोग हुआ है। उन धागों के लिए किस प्रकार के तन्तुओं (फाइवर्स) का प्रयोग किया गया है। वस्त्र कैनवास जैसा मजबूत है, रेशम जैसा भड़कीला है, टेरेलीन जैसा लुभावना है, ऊन जैसा गर्म है, मखमल जैसा आरामदेह है या मलमल जैसा हलका एवं मुलायम है, यह सब विशेषताएं उसके लिये प्रयुक्त धागों एवं उसके तन्तुओं के आधार पर टिकी रहती हैं।
इसी तरह शरीर भी अनेक प्रकार की विशेषताओं से युक्त होते हैं। बन्दर एवं हिरन जैसा फुर्तीला, सिंह एवं हाथी जैसा बलशाली, बैल एवं घोड़े जैसा परिश्रमी, गैंडे जैसा कठोर, हंस जैसा सौम्य, सर्प जैसा लचकदार आदि अनेक प्रकार की विशेषतायें शरीरों में पाई जाती हैं, अथवा पैदा की जा सकती हैं। वह बहुत स्थूल वर्गीकरण है। इससे थोड़े सूक्ष्म स्तर पर देखें तो, ध्रुव प्रदेश एवं हिमालय की ठंड का स्वाभाविक रूप से सहन कर सकने वाले शरीर भूमध्य रेखा के निकट प्रदेशों की भीषण गर्मी में सुखी रहने वाले शरीर, जल जीवों की तरह पानी के संसर्ग में रहने वालों से लेकर मरुभूमि के शुष्कतम वातावरण में निवास करने वाले शरीरों की अपनी-अपनी विशेषताएं उनकी सैल इकाइयों के अनुरूप ही विकसित होती हैं।
शरीर-विज्ञान की अन्तरंग शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि हृदय, आमाशय, आंख, कान, त्वचा आदि तो यन्त्र हैं। इन यन्त्रों के संचालक सूक्ष्म अवयव अन्य ही होते हैं और उन संचालक तत्वों या अवयवों के स्वरूप पर ही हमारे स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार निर्भर रहता है। इन सूक्ष्म अवयवों में हारमोनों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता-निष्क्रियता का हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों पर भारी प्रभाव पड़ता है। शरीर की आकृति कैसी भी हो, उसकी प्रकृति का निर्माण तो मुख्यतः इन हारमोन रसों से ही प्रभावित होता है। यद्यपि आकृति पर भी इन जीवनरस-स्रावों का प्रभाव पड़ता ही है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि विशेष मनःस्थिति के कारण किन्हीं युवतियों का रूप लावण्य तब तक बना रहा, जिस आयु में सामान्य रूप से शरीर पर वृद्धता के चिन्ह उभर आते हैं। उनके बने रहने का रहस्य-सूत्र भी निश्चय ही इन हारमोन-स्रावों में छिपा हुआ माना जाता है। यद्यपि औषधि विद्या और शल्य-प्रक्रिया की पहुंच अभी वहां तक नहीं हो पाई है, पर उनके स्वरूप की कुछ-कुछ जानकारी तो आधुनिक शरीर-शास्त्र को हो ही गई है।
हारमोन स्रावों के विशेष अनुसंधानकर्त्ता डा. क्रुकशेक ने इन स्रावों की आधार ग्रंथियों को ‘जादुई ग्रन्थियां’ कहा है और बताया है कि व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को जानने के लिये इन स्रावों के सन्तुलन और क्रियाकलाप का परीक्षण करके ही यह जाना जा सकता है कि उसका स्तर एवं व्यक्तित्व सचमुच क्या है?
हारमोन वे रासायनिक तत्व या रहस्यमय जीवन रस है, जो अन्तःस्रावी ग्रन्थियों द्वारा स्रवित होते हैं। इन ग्रंथियों की अद्भुत क्षमता के सम्बन्ध में अभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है, उनके बारे में सांकेतिक जानकारी ही प्राप्त हो सकी है। फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि यदि इनके प्रभाव को जाना और नियंत्रित किया जा सके तो मनुष्य अपने भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। अतः स्रावी ग्रन्थियों और उनसे उत्पन्न हारमोनों के आश्चर्यजनक प्रभाव के ढेरों प्रमाण शोधकर्ताओं ने प्राप्त किये हैं।
‘‘एस्ट्रालॉजिकल को रिलेशन्स विद द डक्टलैस ग्लैण्डस्’’ में अन्तःस्रावी ग्रन्थियों की चर्चा आंतरिक ग्रहों के रूप में की गई है। जिस प्रकार सौर-मंडल के विविध ग्रह परस्पर सन्तुलन स्थिति बनाये हैं, वैसे ही ये अन्तःस्रावी ग्रन्थियां शारीरिक, मानसिक सन्तुलन साधे रहती हैं।
इस तुलना-क्रम में सूर्य की पीनियलबाडी से, चन्द्र की पिच्यूटरी से, मंगल की पैराथाइराइड से, बुध की थाइराइड से, बृहस्पति की एड्रीनल से तथा शुक्र की थाइमस से तुलना की गई है। ‘‘आकल्ट एनाटामी’’ के लेखक ने इन ग्रन्थियों का उल्लेख ‘‘ईथर सेन्टर्स’’ के रूप में किया है तथा उनके उद्दीपन को अन्तर्ग्रही चेतना के साथ जोड़ा है। प्रतीत होता है कि अविज्ञात चेतना-केन्द्रों से इन ग्रन्थियों के माध्यम से मनुष्य को कुछ असाधारण अनुदान मिलता रहता है।
उपरोक्त कथानुसार अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड चेतना से—सूक्ष्म जगत से बनता है। वे विश्व शक्तियों के साथ आदान-प्रदान का काम करती है। शरीर-शास्त्र के अनुसार उनका प्रभाव काय-कलेवर के अन्तर्गत शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका अर्थ हुआ कि यह ग्रन्थियां भीतर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व की विविध-विधि क्षमताएं उभारने में असाधारण रूप से होता है। यदि इन ग्रन्थियों को नियन्त्रण से बाहर माना जाता है और समझा जाता है कि इनकी प्रकृति एवं क्रिया-पद्धति बदलना अपने हाथ की बात नहीं है। किन्तु ऐसा है नहीं। सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाले साधनात्मक प्रयत्नों से इन ग्रन्थियों की स्थिति बदली जा सकती है और अनावश्यक हारमोनों का उत्पादन घटाकर जो उपयोगी हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है। अन्नमय कोश में इन ग्रन्थियों के नियन्त्रण सूत्र माने गये हैं।
यह कार्य अध्यात्म के माध्यम से ही सम्भव है। पिछले दिनों आनुवांशिकी विज्ञान के क्षेत्र में काफी शोध प्रयोग किये गये और पाया गया कि मनुष्य के शरीर मन और व्यक्तित्व को बनाने में ऐसे कारणों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो दुर्भाग्य या सौभाग्य की तरह बहुत पहले से ही पल्ले बंधी होती है और उनसे न पीछा छुड़ाना सम्भव होता है तथा न परिवर्तन पुरुषार्थ का ही प्रतिफल होता है। ऐसे प्रसंगों पर अध्यात्म साधना ही एकमात्र उपाय है, जिनके सहारे वंशानुक्रम एवं संग्रहीत संस्कारों में अभीष्ट परिवर्तन सम्भव हो सकता है। इस दृष्टि से शरीर विज्ञान एवं आरोग्य शास्त्र की अपेक्षा अध्यात्म उपचारों की सामर्थ्य बहुत बढ़ी-चढ़ी है। उनके सहारे शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का ही नहीं स्वभाव, दृष्टिकोण एवं समूचे व्यक्तित्व का ही काया कल्प हो सकता है।
व्यक्तित्व का आधार विज्ञान की दृष्टि में
वंशानुक्रम विज्ञान में अब तक जो शोधों हुई हैं उनके अनुसार सन्तान के व्यक्तित्व का ढांचा बनाने में जो जीन्स काम करते हैं, वे न जाने कितनी पीढ़ियों से चले आते हैं। मातृ कुल और पितृ कुल के सूक्ष्म उत्तराधिकारों से वे बनते हैं। सम्मिश्रण की प्रक्रिया द्वारा वे परम्परागत स्थिरता भी बनाये नहीं रहते, वरन् विचित्र प्रकार से परिचर्चित होकर कुछ से कुछ बन जाते हैं। यदि पीढ़ियों को दोष-मुक्त प्रखर एवं सुसंस्कृत बनाना है तो इस जीन प्रक्रिया को प्रभावित तथा परिवर्तित करना होगा, यह अति कठिन कार्य है। उतनी गहराई तक पहुंच सकने वाला कोई उपाय उपचार अभी तक हाथ नहीं लगा है जो इन सूक्ष्म इकाइयों के ढांचे में सुधार या परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। असमर्थता देखते हुए भी यह कार्य बड़ा आवश्यक है कि जीन्स जैसी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी को हस्तगत किया जाय। अन्यथा परिस्थिति वातावरण, आहार-बिहार, शिक्षा परिष्कार के समस्त साधन जुटाने पर भी व्यक्तित्वों का निर्माण ‘विधि-विधान’ स्तर का ही बना रहेगा। इस सन्दर्भ में आशा की किरण अध्यात्म उपचार में ही खोजी जा सकती है। साधना प्रयत्नों से अन्नमय कोश की अन्तःप्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। उससे जीन्सों की स्थिति बदलने और पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जाती है। इतना ही नहीं पैतृक प्रभाव के कारण वयस्क व्यक्ति का जो ढांचा बन गया है उसमें भी सुधार परिष्कार सम्भव हो सकता है। शारीरिक कायाकल्प—मानसिक ब्रेनवाशिंग की चर्चा होती रहती है। व्यक्तित्वों के परिवर्तन में साधनात्मक प्रयोग का परिणाम और भी अधिक उत्साहवर्धक हो सकता है।
आनुवंशिकी खोजों से स्पष्ट हो गया है कि जीन्स में मात्र भोजन की पौष्टिकता का तो प्रभाव नगण्य ही होता है, शारीरिक सुदृढ़ता, स्फूर्ति, अभ्यास, कर्म-कौशल, व्यवहार, विकास, चरित्र का स्तर, मस्तिष्कीय क्षमताओं के विकास आदि सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सारभूत अंश उनमें विद्यमान रहता है। शरीर की विकृतियों का भी वे कारण होते हैं, पर उससे अनेक गुना महत्वपूर्ण तो मनःस्थिति, बौद्धिक क्षमताएं और चारित्रिक प्रवृत्तियां होती हैं। आलस्य और प्रमाद के कारण व्यक्तित्व की क्षमतायें, प्रखरताएं बिखरती, नष्ट होती रहीं, तो शारीरिक सुघड़ता में तो दोष आते ही हैं, व्यक्तित्व का मूलभूत स्तर घटिया होता जाता है। जिससे स्वयं का जीवन भी देवोपम विभूतियों से वंचित रहा जाता है और अपनी सन्तान पर भी उसका विषाक्त प्रभाव छोड़ने का अपराधी बनना पड़ता है।
आनुवंशिकी शोधें इतना भर विश्वास दिलाती हैं कि उपयुक्त रक्त मिश्रण से नई पीढ़ी का विकास हो सकता है। आरोपण प्रत्यारोपण की सम्भावना भी स्वीकार की गई है। वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए नहीं भावी में सुधार होने के सम्बन्ध में ही यह आश्वासन लागू होता है। वैज्ञानिक कहते हैं—‘जीन’ सामान्यतया निष्क्रिय स्थिति में पड़े रहते हैं। उनकी सक्रियता नर-नारी का संगम होने के उपरान्त उभरती हैं। जीन का कार्य युग्म रूप में आरम्भ होता है। जिनका एक सदस्य पिता से आता है और दूसरा माता से। यह जोड़ा मिल कर नई संरचना की विधि-व्यवस्था में जुटता है। यदि दोनों पक्ष एक प्रकृति के हुए तो उनका सृजन ठीक उसी रूप में होगा, किन्तु यदि भिन्नता रही तो दोनों के सम्मिश्रण का जो परिणाम होगा वह सामने आवेगा। जो पक्ष प्रबल (डामिनेन्ट) होगा वह दुर्बल पक्ष—(रिसेसिव) की विशेषताओं को दबा कर अपना वर्चस्व प्रकट करेगा। फिर भी दुर्बल पक्ष की कुछ विशेषताएं तो उस नए सम्मिश्रित सृजन में दृष्टिगोचर होती रहेंगी। एकरूपता मिलते चलने पर आकार भार बढ़ेगा। पानी में पानी मिलाते चलने पर रहेगा पानी ही, उसका परिमाण भर बढ़ेगा। किन्तु दो भिन्नताएं मिलकर आकार ही नहीं स्थिति और प्रकृति का परिवर्तन भी प्रस्तुत करेगी। पीला और नीला रंग मिला देने पर वे दोनों ही अपना मूल स्वरूप खो बैठेंगे और तीसरा नया हरा रंग बन जायगा। जीनों की परम्परा में पाई जाने वाली विशेषता यों तथ्य रूप तो बनी रहेगी, पर उसका प्रत्यक्ष रूप परिवर्तित दृष्टिगोचर होगा। घोड़ी और गधे के सम्मिश्रण से नई किस्म के खच्चर पैदा होते हैं। कलमी पौधों के फल-फूलों में नये किस्म की विशेषताएं उभरती हैं।
आनुवंशिकी के आधार पर अब तक इतना ही सम्भव हो सका है कि उपयुक्त जोड़े मिला कर भावी पीढ़ी के विकास की बात सोची जाय। उस क्षेत्र में भी यह प्रश्न बना हुआ है कि निर्धारित जोड़े में जो विकृतियां चली आ रही होंगी उनका निवारण, निष्कासन कैसे होगा? अच्छाई अच्छाई से मिल कर अच्छा परिणाम उत्पन्न कर सकती है तो बुराई बुराई से मिलकर अधिक बुराई क्यों उत्पन्न न करेगी? यदि अच्छाई-बुराई के बीच संघर्ष आरम्भ हो गया तो नई मध्यवर्ती स्थिति बन सकती है, पर प्रगति का अभीष्ट परिणाम किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगा?
आनुवंशिकी शोधें तथ्यों पर पड़े पर्दे का तो उद्घाटन करती हैं पर अभीष्ट सुधार के लिए उपयुक्त एवं सुनिश्चित मार्ग-दर्शन करना उनके लिए भी सम्भव नहीं हो सका है। वनस्पति में प्रत्यारोपण किया के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। कृत्रिम गर्भाधान तथा दूसरे प्रत्यारोपणों का परिणाम भी किसी कदर अच्छा निकला है। मनुष्य की शरीर रचना में भी थोड़े हेर-फेर हुए हैं। गोरे और काले पति-पत्नी के संयोग से तीसरी आकृति बनी है। एंग्लोइण्डियन रेस अपने ढंग की अलग ही है। इतने पर भी मूल समस्या जहां की तहां है। जीन के साथ जुड़ी हुई पैतृत्व परम्परा में जो रोग अथवा दुःस्वभाव जुड़े रहेंगे उनको हटाना या मिटाना कैसे बन पड़ेगा? यह तो भावी पीढ़ी के परिवर्तन में प्रस्तुत कठिनाई हुई। प्रधान बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी को अवांछनीय उत्तराधिकार से किस प्रकार छुटकारा दिलाया जाय? उसे असहाय स्थिति में पड़े रहने की विवशता से त्राण पाने का अवसर कैसे मिले? इस क्षेत्र में परिवर्तन हो सकने की बात बहुत ही कठिन मालूम देती है।
मनुष्य के एक जीन में करोड़ों इकाइयां होती हैं। इन पर विषाणुओं, वायरसों की क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रस्तुत शोधें इसी उपक्रम के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। डा. हरगोविन्द सिंह खुराना ने जिस जीन के कृत्रिम संश्लेषण में सफलता प्राप्त करके नोबुल पुरस्कार जीता था, वह मात्र 199 इकाइयों को सही क्रम से जोड़ने में 9 वर्ष लगे हैं। यह तो एक प्रयोग भर हुआ। मनुष्य के एक जीन में पाई जाने वाली करोड़ों इकाइयों को सही क्रम से जोड़ना अतीव दुष्कर है। यहां एक बात और भी ध्यान रखने की है कि प्रत्येक जीवाणु कोशिका में ऐसे कई लाख जीन होते हैं। जो मानव शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के निर्माण एवं संचालन का कार्य सम्पन्न करते हैं।
शरीर के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों के जीन्स द्वारा निर्माण की प्रक्रिया को अनुशासित रखने का दायित्व ‘एन्जाइमों’ का है। ये ‘एन्जाइम’ न्यूक्लिक अम्लों के माध्यम से—जीन्स से सम्बद्ध रहते हैं। चुम्बकत्व-शक्ति के प्रयोगों—उपचारों द्वारा इन एन्जाइमों को प्रभावित कर जीन्स के विकास-क्रम पर प्रभाव डाला जा सकता है। अभी वैज्ञानिक इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं।
भारत में अतीतकाल में सुसन्तति के लिये तप-साधना का विधान था, जो कि मनुष्य में अन्तर्निहित चुम्बकत्व-शक्ति का विकास-अभिवर्धन करता था। कृष्ण और रुक्मिणी ने बद्रीनाथ धाम में बारह वर्ष तक तप कर अपनी चुम्बकत्व-शक्ति को अत्यधिक उत्कृष्ट बना लिया था। तभी उन्हें प्रद्युम्न के रूप में मनोवांछित सन्तान प्राप्त हो सकी थी। वैज्ञानिकों का मत है कि जीन्स की विशेषताएं विकिरणों द्वारा प्रभावित की जा सकती हैं। शरीर के भीतर रश्मियों के केन्द्रीयकरण द्वारा ऐसी विकिरण-चिकित्सा व्यवस्था की जा सकती है। विद्युत-क्षेत्र (इलेक्ट्रिक-फील्ड्स) द्वारा जीन्स की रासायनिक और विद्युतीय दोनों विशेषताओं में परिमार्जन संशोधन किये जा सकते हैं। ध्वनियों तथा अतिध्वनियों के क्षेत्र में भी खोजें चल रही हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनके द्वारा भी जीन्स में परिवर्तन की विधि खोजी जा सकती है।
भौतिक विज्ञान से यह सम्भव हो या न हो, पर अध्यात्म विज्ञान से तो यह साध्य है ही। भारतवर्ष में साधना द्वारा शरीरस्थ जैवीय विद्युत को प्रखर बना कर मन्त्रों के माध्यम से उत्पन्न अतिध्वनियों तथा यज्ञादि के विकिरण का उपयोग इस दिशा में सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। इन्द्र को जीतने में समर्थ वृत्रासुर की उत्पत्ति तथा राजा दशरथ के यहां राम भरत जैसी सुसन्तति की प्राप्ति ऐसे ही प्रयोगों द्वारा सम्भव हुई थी।
अध्यात्म विज्ञान वहां से आरम्भ होता है जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं प्रायः समाप्त हो जाती हैं। स्थूल की अगली सीढ़ी सूक्ष्म है। अन्तःस्रावी ग्रन्थियों से निकलने वाले विचित्र हारमोन स्रावों की तरह आनुवंशिकी क्षेत्र के रहस्यमय घटक ‘जीन’ भी उतने ही विलक्षण हैं। इन्हें प्रभावित करने में, भौतिकी सफल न हो सके तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। सुनियोजित अध्यात्म विज्ञान के पीछे वे सम्भावनाएं झांकती हैं जिससे न केवल हारमोन और जीन वरन् ऐसे-ऐसे अनेकों रहस्यमय केन्द्र प्रभावित परिष्कृत किये जा सकते हैं जो सामान्य मनुष्य जीवन को असामान्य—देवोपम बना सकने में समर्थ हैं। अध्यात्म विज्ञान की ‘अन्नमय कोश’ की कक्षा-प्रयोग प्रक्रिया इसी उद्देश्य को पूरा करती है।
अन्नमय कोश के सूक्ष्म घटक
अन्नमय कोश के बाह्यावरण से आगे चलकर इसका अध्ययन किया जाय तो इसका स्वरूप सूक्ष्म क्षमताओं से भरा हुआ उभर कर सामने आयेगा किसी भी क्षेत्र में उच्चस्तरीय साधक का सारा शरीर उसकी मुख्य साधना में सहयोगी बन जाता है। श्रेष्ठ चित्रकार जब किसी चित्र की कल्पना करता है तो इसके शरीर की हर इकाई इसके स्पंदनों से प्रभावित होती है। शरीर की हलचल में उस कल्पना के स्पंदन समाविष्य हो जाते हैं तथा निर्जीव तूलिका सामान्य रंगों में ही जीवंत चित्र का निर्माण कर देती है। वाणी के साधक गायक के मन में जो भाव उभरते हैं वह उसके हाव-भाव तथा स्वर लहरी में न जाने कहां से—कैसे गुंथ जाते हैं और उसमें अद्भुत प्रभाव पैदा कर देते हैं। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान चिकित्सक के चर्मचक्षुओं और मांस-पेशियों में न जाने क्या विशेषता आ जाती है कि वह रोग के सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह तथा गम्भीर से गम्भीर स्तर को पकड़ लेता है। इन साधकों के चमत्कारों के पीछे यही तथ्य छिपा है कि उनके अन्नमय कोश की हर इकाई उनके अन्दर की सूक्ष्म सम्वेदनाओं को अनुभव करने, स्वीकार करने तथा उसके अनुरूप प्रभाव पैदा करने में सक्षम हो जाती है। उसके संस्कार उसके अनुरूप हो जाते हैं। किसी भी उच्चस्तरीय साधना के लिये विज्ञान से लेकर उपासना तक के लिये अपने अन्नमय कोश को ऐसी ही सुसंस्कृत, सुयोग्य, सक्षम स्थिति में लाना आवश्यक होता है। उसके लिये उसकी मूल इकाइयों को विशेष रूप से गढ़ना-ढालना पड़ता है। इसे ही अन्नमय कोश का परिष्कार विकास की साधना कहा जाता है।
प्रश्न उठता है कि क्या अन्नमय कोश की मूल इकाइयों को वांछित ढंग का बनाया जा सकता है? हां, यह सम्भव है। इसकी पुष्टि भारतीय दर्शन की सनातन मान्यता तथा वर्तमान वैज्ञानिक शोधों, दोनों ही आधारों पर होती है। वस्त्र आदि तो जैसे बन गये वैसे बन गये कैनवास को मखमल में नहीं बदला जा सकता। क्योंकि वह जड़ संस्थान है। किन्तु शरीर तो चेतन संस्थान है। उसमें नये कोशों का निर्माण तथा पुरानों का विघटन सम्भव ही नहीं है, वह तो उसकी एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धीमी पड़ने से ही मनुष्य शरीर जराजीर्ण होने लगता है। जरा बुढ़ापा कुछ और नहीं अन्नमय कोश में नवीन स्वस्थ कोशिकाओं की संरचना तथा पुरानों के निष्कासन की गति शिथिल हो जाना मात्र है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित, नियमित बनाकर शरीर संस्थान में क्रमशः इच्छित परिवर्तन लाये जा सकते हैं।
सामान्य व्यक्तियों में भी अन्नमय कोश की इकाइयों में परिवर्तन होता ही रहता है। किन्तु उसकी कोई व्यवस्था, योजना न होने के कारण एक ढर्रा भर चलता रहता है। सामान्य रूप से किसी भी फैक्ट्री में पुराने पुर्जों तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नये पुर्जे एवं नई मशीनों को स्थापित करने का क्रम चलता ही रहता है। उससे एक ढर्रे का उत्पादन निकलता भी रहता है। किन्तु कोई कुशल शिल्पी-उद्योगी जब अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाने, नयी वस्तुएं उत्पादित करने की योजना बनाता है तो फिर ढर्रे का क्रम पर्याप्त नहीं। उस स्थिति में लक्ष्य को ध्यान में रखकर सूझबूझ के साथ हर परिवर्तन व्यवस्थित ढंग से करना होता है। पुर्जों और मशीनों से लेकर औजार (टूल) तथा कच्चे माल की व्यवस्था भी उसी योजना के अनुरूप करनी होती है। अपने शरीर की हर कोशिका को एक सजीव पुर्जा, औजार, मशीन मानकर उन्हें लक्ष्य के अनुरूप बनाना, उसके लिये उपयुक्त आहार विहार अपनाना, योग साधक के लिये आवश्यक हो जाता है।
सामान्य व्यक्ति के अन्नमय कोश तथा योगी के अन्नमय कोश में अन्तर क्यों? किस आधार पर आवश्यक है? इसे एक सामान्य उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बिजली की लाइन को लें। विद्युत तारों में बहती है। उन्हें सहारा देने के लिये खम्भे रहते हैं। तार और खम्भों के बीच में ऐसे उपकरण लगे रहते हैं जो बिजली को खम्भों में होकर पृथ्वी में प्रविष्ट होने से रोके रहें। उन्हें ‘कुचालक इन्सुलेटर’ सामान्य दबाव (वोल्टेज) की विद्युत के लिये तार खम्भे तथा इन्सुलेटर सामान्य ही चल जाते हैं। किन्तु यदि ऊंचे दबाव (हाईवोल्टेज) की बिजली अधिक मात्रा में प्रवाहित करनी हो तो उसके लिए यह सभी उपकरण विशिष्ट स्तर के लगाने पड़ते हैं। यही बात सामान्य व्यक्ति तथा विशिष्ट साधक के साथ लागू होती है। सामान्य जीवनक्रम में सामान्य शारीरिक जैवीय विद्युत (बायो इलेक्ट्रिसिटी) की ही आवश्यकता पड़ती है, किन्तु उच्च लक्ष्यों के लिये अधिक प्रखर शक्ति तरंगें पैदा करनी होती हैं। उनका सम्वेदन, संचार करने के लिये अधिक सशक्त संस्थान की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़नी ही चाहिये। इसीलिये साधक को अपने अन्नमय कोश के परिष्कार, उसकी पुष्टि और विकास के लिए विशेष ध्यान देना, विशेष प्रयास करना होता है। तभी वह प्राणमय मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोशों के विकास में सहायक बनने तथा उनकी विकसित स्थिति के साथ तेलमेल बिठाने में समर्थ हो पाता है।
ताल-मेल बिठाने की बात यों ही नहीं कही गई है, उसका अपना विशिष्ट अर्थ है। निर्जीव घटक तालमेल नहीं बिठा सकते, वह तो चेतना सम्पन्न के लिए ही सम्भव है। अन्नकोश की हर इकाई, हर कोशिका (सैल) को आज के वैज्ञानिक भी स्वतन्त्र जैविक इकाई मानने लगे हैं। हर सैल में उसका हृदय न्यूक्लियस होता है। उसके श्वांस संस्थान को वैज्ञानिक भाषा में ‘माइटो कौंकिया’ कहते हैं। हर सैल में एक ‘गाल्गी एप्रेटस’ होता है जो उनके पाचन संस्थान का काम करता है। हर कोश अपने जैसे नये कोश का उत्पादन कर सकता है। इस व्यवस्था को वैज्ञानिक ‘न्यूक्लियोलस एण्ड क्रोमेटिन नैटवर्क’ कहते हैं। हर सैल में अपनी एक विशिष्ट जैवीय विद्युत का प्रभार (चार्ज) होती है जिसे उसका प्राण कहते हैं। इस प्रकार हर कोशिका एक स्वतन्त्र जैविक इकाई के रूप में अपने अस्तित्व को बनाये रखते हुए, शरीर संस्थान से अपना तालमेल बिठाये रखता है।
अन्नमय कोश के कोटि-कोटि सदस्य यह कोशिकाएं (सैल) इस उद्देश्य-लक्ष्य के अनुरूप स्वयं में स्वाभाविक क्षमता उत्पन्न कर सकें, उसके लिये विशिष्ट संस्कारवान नयी कोशिकाओं का उत्पादन कर सकें, तो उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति की सुनिश्चित पृष्ठभूमि बन जाती है। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से—योजनाबद्ध प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। उनके लिये आहार, विहार, चिन्तन आदि की विशिष्ट एवं व्यवस्थित पद्धति का अनुकरण करना होता है। जैसे बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए उन्हें साधन ही नहीं श्रेष्ठ संस्कार भी देने पड़ते हैं, इसी प्रकार इन कोशिकाओं के लिए भी आहार व्यवहार से लेकर ध्यान उपासना तक के अनेक माध्यम अपनाने होते हैं। उन सबके संयोग से ही अन्नमय कोश की प्रभावशाली साधना का स्वरूप बनता है।
यह सब उपलब्धियां आध्यात्मिक साधना मार्ग पर बढ़ने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है और सांसारिक जीवनक्रम में भी इनका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। यह उपलब्धियां बड़ी आकर्षक भी लगती हैं। किन्तु योग मार्ग की यह बहुत प्रारम्भिक सीढ़ियां हैं। यह इसलिये आवश्यक है कि योग साधना के लिये आवश्यक साधनाक्रम में यह शरीर अपनी असमर्थता प्रकट करके साथ देने से कतराने न लगे। अन्नमय कोश शुद्ध और पुष्ट होने पर ही व्यक्ति सांसारिक उतार-चढ़ावों के बीच अपनी शरीर यात्रा को सन्तुलित क्रम से चलाता हुआ, अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर अनवरत क्रम से बढ़ सकता है।
एक और सूक्ष्म पक्ष है जिसके लिये अन्नमय कोश को तैयार करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति के क्रम में शरीर में अनेक दिव्य संवेदनाओं का संसार होता है। असंस्कारित अन्नमय कोश उसमें बाधक बन जाता है। अथवा वांछित सहयोग नहीं देने पाता। इस क्रम में अनेक दिव्य क्षमताएं उभरती हैं, उन्हें धारण करना उनके स्पन्दनों को सहन करके अपना सन्तुलन बनाये रखना भी बहुत आवश्यक है। यह सभी बातें परिष्कृत एवं विकसित क्षमता सम्पन्न अन्नमय कोश से ही सम्भव हैं।
इन सब उपलब्धियों एवं क्षमताओं का लाभ पाने के लिये अन्नमय कोश, उसके स्वरूप तथा सामान्य गुण धर्मों के बारे में भी साधक के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप रेखा होनी चाहिये। पांचों कोशों की संगति में अन्नमय कोश की भूमिका तथा उसके महत्व को उचित अनुपात में समझना आवश्यक है।
हमारी सत्ता, स्थूल-सूक्ष्म अनेक स्तर के तत्वों के संयोग से बनी है। उनमें से हर एक घटक का अपना-अपना महत्व है। किसी एक घटक का महत्व बतलाने से किसी दूसरे घटक का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे का सहयोगी पूरक तो है, किन्तु उसका स्थान वह स्वयं नहीं ले सकता। उदाहरण के लिये भवन निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट का गारा (मार्टर) लें। उसमें सीमेंट, बालू, पानी, रंग आदि सभी मिलाये जाते हैं। किसी एक का भी स्तर घटिया हो तो गारा घटिया हो जायेगा। उसकी लोच, मजबूती, सुन्दरता आदि इन सभी के सन्तुलित संयोग से है। हमारे अस्तित्व के बारे में भी यही तथ्य लागू होता है। हमारे अस्तित्व के हर घटक का, हर कोश का अपना-अपना महत्व है। इसीलिये उन सबकी उत्कृष्टता एवं सन्तुलन का ध्यान रखना आवश्यक है।
हमारी संरचना में एक बड़ा भाग वह है जिसका सीधा सम्बन्ध स्थूल पदार्थों—पंच भूतों से है। उसके अस्तित्व, पोषण एवं विकास के लिये स्थूल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर संस्थान के इसी भाग को अन्नमय कोश कहते हैं। यह अगणित छोटी-छोटी स्थूल इकाईयों से बना हुआ है। इन्हें कोशिका (सैल) कहते हैं। स्पष्ट है कि यह इकाइयां जिस प्रकार की, जिन गुण धर्मों से युक्त होगी, संयुक्त शरीर संस्थान में भी वही गुण धर्म प्रकट होंगे। उन मूल इकाइयों को बदले बिना बाह्य दृश्य संस्थान में इच्छित विशेषताएं पैदा नहीं की जा सकतीं। अन्नमय कोश को आवश्यकता के अनुरूप बनाने ढालने के लिये भी उसकी मूल इकाइयों को ध्यान में रखना होगा।
उदाहरण के लिये कोई वस्त्र लें। वस्त्र किस कोटि का है, यह इस आधार पर निर्भर करता है उसकी रचना में किस प्रकार के धागों का उपयोग हुआ है। उन धागों के लिए किस प्रकार के तन्तुओं (फाइवर्स) का प्रयोग किया गया है। वस्त्र कैनवास जैसा मजबूत है, रेशम जैसा भड़कीला है, टेरेलीन जैसा लुभावना है, ऊन जैसा गर्म है, मखमल जैसा आरामदेह है या मलमल जैसा हलका एवं मुलायम है, यह सब विशेषताएं उसके लिये प्रयुक्त धागों एवं उसके तन्तुओं के आधार पर टिकी रहती हैं।
इसी तरह शरीर भी अनेक प्रकार की विशेषताओं से युक्त होते हैं। बन्दर एवं हिरन जैसा फुर्तीला, सिंह एवं हाथी जैसा बलशाली, बैल एवं घोड़े जैसा परिश्रमी, गैंडे जैसा कठोर, हंस जैसा सौम्य, सर्प जैसा लचकदार आदि अनेक प्रकार की विशेषतायें शरीरों में पाई जाती हैं, अथवा पैदा की जा सकती हैं। वह बहुत स्थूल वर्गीकरण है। इससे थोड़े सूक्ष्म स्तर पर देखें तो, ध्रुव प्रदेश एवं हिमालय की ठंड का स्वाभाविक रूप से सहन कर सकने वाले शरीर भूमध्य रेखा के निकट प्रदेशों की भीषण गर्मी में सुखी रहने वाले शरीर, जल जीवों की तरह पानी के संसर्ग में रहने वालों से लेकर मरुभूमि के शुष्कतम वातावरण में निवास करने वाले शरीरों की अपनी-अपनी विशेषताएं उनकी सैल इकाइयों के अनुरूप ही विकसित होती हैं।
शरीर-विज्ञान की अन्तरंग शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि हृदय, आमाशय, आंख, कान, त्वचा आदि तो यन्त्र हैं। इन यन्त्रों के संचालक सूक्ष्म अवयव अन्य ही होते हैं और उन संचालक तत्वों या अवयवों के स्वरूप पर ही हमारे स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार निर्भर रहता है। इन सूक्ष्म अवयवों में हारमोनों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता-निष्क्रियता का हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों पर भारी प्रभाव पड़ता है। शरीर की आकृति कैसी भी हो, उसकी प्रकृति का निर्माण तो मुख्यतः इन हारमोन रसों से ही प्रभावित होता है। यद्यपि आकृति पर भी इन जीवनरस-स्रावों का प्रभाव पड़ता ही है। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि विशेष मनःस्थिति के कारण किन्हीं युवतियों का रूप लावण्य तब तक बना रहा, जिस आयु में सामान्य रूप से शरीर पर वृद्धता के चिन्ह उभर आते हैं। उनके बने रहने का रहस्य-सूत्र भी निश्चय ही इन हारमोन-स्रावों में छिपा हुआ माना जाता है। यद्यपि औषधि विद्या और शल्य-प्रक्रिया की पहुंच अभी वहां तक नहीं हो पाई है, पर उनके स्वरूप की कुछ-कुछ जानकारी तो आधुनिक शरीर-शास्त्र को हो ही गई है।
हारमोन स्रावों के विशेष अनुसंधानकर्त्ता डा. क्रुकशेक ने इन स्रावों की आधार ग्रंथियों को ‘जादुई ग्रन्थियां’ कहा है और बताया है कि व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को जानने के लिये इन स्रावों के सन्तुलन और क्रियाकलाप का परीक्षण करके ही यह जाना जा सकता है कि उसका स्तर एवं व्यक्तित्व सचमुच क्या है?
हारमोन वे रासायनिक तत्व या रहस्यमय जीवन रस है, जो अन्तःस्रावी ग्रन्थियों द्वारा स्रवित होते हैं। इन ग्रंथियों की अद्भुत क्षमता के सम्बन्ध में अभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है, उनके बारे में सांकेतिक जानकारी ही प्राप्त हो सकी है। फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि यदि इनके प्रभाव को जाना और नियंत्रित किया जा सके तो मनुष्य अपने भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। अतः स्रावी ग्रन्थियों और उनसे उत्पन्न हारमोनों के आश्चर्यजनक प्रभाव के ढेरों प्रमाण शोधकर्ताओं ने प्राप्त किये हैं।
‘‘एस्ट्रालॉजिकल को रिलेशन्स विद द डक्टलैस ग्लैण्डस्’’ में अन्तःस्रावी ग्रन्थियों की चर्चा आंतरिक ग्रहों के रूप में की गई है। जिस प्रकार सौर-मंडल के विविध ग्रह परस्पर सन्तुलन स्थिति बनाये हैं, वैसे ही ये अन्तःस्रावी ग्रन्थियां शारीरिक, मानसिक सन्तुलन साधे रहती हैं।
इस तुलना-क्रम में सूर्य की पीनियलबाडी से, चन्द्र की पिच्यूटरी से, मंगल की पैराथाइराइड से, बुध की थाइराइड से, बृहस्पति की एड्रीनल से तथा शुक्र की थाइमस से तुलना की गई है। ‘‘आकल्ट एनाटामी’’ के लेखक ने इन ग्रन्थियों का उल्लेख ‘‘ईथर सेन्टर्स’’ के रूप में किया है तथा उनके उद्दीपन को अन्तर्ग्रही चेतना के साथ जोड़ा है। प्रतीत होता है कि अविज्ञात चेतना-केन्द्रों से इन ग्रन्थियों के माध्यम से मनुष्य को कुछ असाधारण अनुदान मिलता रहता है।
उपरोक्त कथानुसार अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड चेतना से—सूक्ष्म जगत से बनता है। वे विश्व शक्तियों के साथ आदान-प्रदान का काम करती है। शरीर-शास्त्र के अनुसार उनका प्रभाव काय-कलेवर के अन्तर्गत शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका अर्थ हुआ कि यह ग्रन्थियां भीतर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व की विविध-विधि क्षमताएं उभारने में असाधारण रूप से होता है। यदि इन ग्रन्थियों को नियन्त्रण से बाहर माना जाता है और समझा जाता है कि इनकी प्रकृति एवं क्रिया-पद्धति बदलना अपने हाथ की बात नहीं है। किन्तु ऐसा है नहीं। सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाले साधनात्मक प्रयत्नों से इन ग्रन्थियों की स्थिति बदली जा सकती है और अनावश्यक हारमोनों का उत्पादन घटाकर जो उपयोगी हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है। अन्नमय कोश में इन ग्रन्थियों के नियन्त्रण सूत्र माने गये हैं।
यह कार्य अध्यात्म के माध्यम से ही सम्भव है। पिछले दिनों आनुवांशिकी विज्ञान के क्षेत्र में काफी शोध प्रयोग किये गये और पाया गया कि मनुष्य के शरीर मन और व्यक्तित्व को बनाने में ऐसे कारणों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो दुर्भाग्य या सौभाग्य की तरह बहुत पहले से ही पल्ले बंधी होती है और उनसे न पीछा छुड़ाना सम्भव होता है तथा न परिवर्तन पुरुषार्थ का ही प्रतिफल होता है। ऐसे प्रसंगों पर अध्यात्म साधना ही एकमात्र उपाय है, जिनके सहारे वंशानुक्रम एवं संग्रहीत संस्कारों में अभीष्ट परिवर्तन सम्भव हो सकता है। इस दृष्टि से शरीर विज्ञान एवं आरोग्य शास्त्र की अपेक्षा अध्यात्म उपचारों की सामर्थ्य बहुत बढ़ी-चढ़ी है। उनके सहारे शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का ही नहीं स्वभाव, दृष्टिकोण एवं समूचे व्यक्तित्व का ही काया कल्प हो सकता है।
व्यक्तित्व का आधार विज्ञान की दृष्टि में
वंशानुक्रम विज्ञान में अब तक जो शोधों हुई हैं उनके अनुसार सन्तान के व्यक्तित्व का ढांचा बनाने में जो जीन्स काम करते हैं, वे न जाने कितनी पीढ़ियों से चले आते हैं। मातृ कुल और पितृ कुल के सूक्ष्म उत्तराधिकारों से वे बनते हैं। सम्मिश्रण की प्रक्रिया द्वारा वे परम्परागत स्थिरता भी बनाये नहीं रहते, वरन् विचित्र प्रकार से परिचर्चित होकर कुछ से कुछ बन जाते हैं। यदि पीढ़ियों को दोष-मुक्त प्रखर एवं सुसंस्कृत बनाना है तो इस जीन प्रक्रिया को प्रभावित तथा परिवर्तित करना होगा, यह अति कठिन कार्य है। उतनी गहराई तक पहुंच सकने वाला कोई उपाय उपचार अभी तक हाथ नहीं लगा है जो इन सूक्ष्म इकाइयों के ढांचे में सुधार या परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। असमर्थता देखते हुए भी यह कार्य बड़ा आवश्यक है कि जीन्स जैसी व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी को हस्तगत किया जाय। अन्यथा परिस्थिति वातावरण, आहार-बिहार, शिक्षा परिष्कार के समस्त साधन जुटाने पर भी व्यक्तित्वों का निर्माण ‘विधि-विधान’ स्तर का ही बना रहेगा। इस सन्दर्भ में आशा की किरण अध्यात्म उपचार में ही खोजी जा सकती है। साधना प्रयत्नों से अन्नमय कोश की अन्तःप्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। उससे जीन्सों की स्थिति बदलने और पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जाती है। इतना ही नहीं पैतृक प्रभाव के कारण वयस्क व्यक्ति का जो ढांचा बन गया है उसमें भी सुधार परिष्कार सम्भव हो सकता है। शारीरिक कायाकल्प—मानसिक ब्रेनवाशिंग की चर्चा होती रहती है। व्यक्तित्वों के परिवर्तन में साधनात्मक प्रयोग का परिणाम और भी अधिक उत्साहवर्धक हो सकता है।
आनुवंशिकी खोजों से स्पष्ट हो गया है कि जीन्स में मात्र भोजन की पौष्टिकता का तो प्रभाव नगण्य ही होता है, शारीरिक सुदृढ़ता, स्फूर्ति, अभ्यास, कर्म-कौशल, व्यवहार, विकास, चरित्र का स्तर, मस्तिष्कीय क्षमताओं के विकास आदि सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सारभूत अंश उनमें विद्यमान रहता है। शरीर की विकृतियों का भी वे कारण होते हैं, पर उससे अनेक गुना महत्वपूर्ण तो मनःस्थिति, बौद्धिक क्षमताएं और चारित्रिक प्रवृत्तियां होती हैं। आलस्य और प्रमाद के कारण व्यक्तित्व की क्षमतायें, प्रखरताएं बिखरती, नष्ट होती रहीं, तो शारीरिक सुघड़ता में तो दोष आते ही हैं, व्यक्तित्व का मूलभूत स्तर घटिया होता जाता है। जिससे स्वयं का जीवन भी देवोपम विभूतियों से वंचित रहा जाता है और अपनी सन्तान पर भी उसका विषाक्त प्रभाव छोड़ने का अपराधी बनना पड़ता है।
आनुवंशिकी शोधें इतना भर विश्वास दिलाती हैं कि उपयुक्त रक्त मिश्रण से नई पीढ़ी का विकास हो सकता है। आरोपण प्रत्यारोपण की सम्भावना भी स्वीकार की गई है। वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए नहीं भावी में सुधार होने के सम्बन्ध में ही यह आश्वासन लागू होता है। वैज्ञानिक कहते हैं—‘जीन’ सामान्यतया निष्क्रिय स्थिति में पड़े रहते हैं। उनकी सक्रियता नर-नारी का संगम होने के उपरान्त उभरती हैं। जीन का कार्य युग्म रूप में आरम्भ होता है। जिनका एक सदस्य पिता से आता है और दूसरा माता से। यह जोड़ा मिल कर नई संरचना की विधि-व्यवस्था में जुटता है। यदि दोनों पक्ष एक प्रकृति के हुए तो उनका सृजन ठीक उसी रूप में होगा, किन्तु यदि भिन्नता रही तो दोनों के सम्मिश्रण का जो परिणाम होगा वह सामने आवेगा। जो पक्ष प्रबल (डामिनेन्ट) होगा वह दुर्बल पक्ष—(रिसेसिव) की विशेषताओं को दबा कर अपना वर्चस्व प्रकट करेगा। फिर भी दुर्बल पक्ष की कुछ विशेषताएं तो उस नए सम्मिश्रित सृजन में दृष्टिगोचर होती रहेंगी। एकरूपता मिलते चलने पर आकार भार बढ़ेगा। पानी में पानी मिलाते चलने पर रहेगा पानी ही, उसका परिमाण भर बढ़ेगा। किन्तु दो भिन्नताएं मिलकर आकार ही नहीं स्थिति और प्रकृति का परिवर्तन भी प्रस्तुत करेगी। पीला और नीला रंग मिला देने पर वे दोनों ही अपना मूल स्वरूप खो बैठेंगे और तीसरा नया हरा रंग बन जायगा। जीनों की परम्परा में पाई जाने वाली विशेषता यों तथ्य रूप तो बनी रहेगी, पर उसका प्रत्यक्ष रूप परिवर्तित दृष्टिगोचर होगा। घोड़ी और गधे के सम्मिश्रण से नई किस्म के खच्चर पैदा होते हैं। कलमी पौधों के फल-फूलों में नये किस्म की विशेषताएं उभरती हैं।
आनुवंशिकी के आधार पर अब तक इतना ही सम्भव हो सका है कि उपयुक्त जोड़े मिला कर भावी पीढ़ी के विकास की बात सोची जाय। उस क्षेत्र में भी यह प्रश्न बना हुआ है कि निर्धारित जोड़े में जो विकृतियां चली आ रही होंगी उनका निवारण, निष्कासन कैसे होगा? अच्छाई अच्छाई से मिल कर अच्छा परिणाम उत्पन्न कर सकती है तो बुराई बुराई से मिलकर अधिक बुराई क्यों उत्पन्न न करेगी? यदि अच्छाई-बुराई के बीच संघर्ष आरम्भ हो गया तो नई मध्यवर्ती स्थिति बन सकती है, पर प्रगति का अभीष्ट परिणाम किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगा?
आनुवंशिकी शोधें तथ्यों पर पड़े पर्दे का तो उद्घाटन करती हैं पर अभीष्ट सुधार के लिए उपयुक्त एवं सुनिश्चित मार्ग-दर्शन करना उनके लिए भी सम्भव नहीं हो सका है। वनस्पति में प्रत्यारोपण किया के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। कृत्रिम गर्भाधान तथा दूसरे प्रत्यारोपणों का परिणाम भी किसी कदर अच्छा निकला है। मनुष्य की शरीर रचना में भी थोड़े हेर-फेर हुए हैं। गोरे और काले पति-पत्नी के संयोग से तीसरी आकृति बनी है। एंग्लोइण्डियन रेस अपने ढंग की अलग ही है। इतने पर भी मूल समस्या जहां की तहां है। जीन के साथ जुड़ी हुई पैतृत्व परम्परा में जो रोग अथवा दुःस्वभाव जुड़े रहेंगे उनको हटाना या मिटाना कैसे बन पड़ेगा? यह तो भावी पीढ़ी के परिवर्तन में प्रस्तुत कठिनाई हुई। प्रधान बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी को अवांछनीय उत्तराधिकार से किस प्रकार छुटकारा दिलाया जाय? उसे असहाय स्थिति में पड़े रहने की विवशता से त्राण पाने का अवसर कैसे मिले? इस क्षेत्र में परिवर्तन हो सकने की बात बहुत ही कठिन मालूम देती है।
मनुष्य के एक जीन में करोड़ों इकाइयां होती हैं। इन पर विषाणुओं, वायरसों की क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रस्तुत शोधें इसी उपक्रम के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। डा. हरगोविन्द सिंह खुराना ने जिस जीन के कृत्रिम संश्लेषण में सफलता प्राप्त करके नोबुल पुरस्कार जीता था, वह मात्र 199 इकाइयों को सही क्रम से जोड़ने में 9 वर्ष लगे हैं। यह तो एक प्रयोग भर हुआ। मनुष्य के एक जीन में पाई जाने वाली करोड़ों इकाइयों को सही क्रम से जोड़ना अतीव दुष्कर है। यहां एक बात और भी ध्यान रखने की है कि प्रत्येक जीवाणु कोशिका में ऐसे कई लाख जीन होते हैं। जो मानव शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के निर्माण एवं संचालन का कार्य सम्पन्न करते हैं।
शरीर के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों के जीन्स द्वारा निर्माण की प्रक्रिया को अनुशासित रखने का दायित्व ‘एन्जाइमों’ का है। ये ‘एन्जाइम’ न्यूक्लिक अम्लों के माध्यम से—जीन्स से सम्बद्ध रहते हैं। चुम्बकत्व-शक्ति के प्रयोगों—उपचारों द्वारा इन एन्जाइमों को प्रभावित कर जीन्स के विकास-क्रम पर प्रभाव डाला जा सकता है। अभी वैज्ञानिक इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं।
भारत में अतीतकाल में सुसन्तति के लिये तप-साधना का विधान था, जो कि मनुष्य में अन्तर्निहित चुम्बकत्व-शक्ति का विकास-अभिवर्धन करता था। कृष्ण और रुक्मिणी ने बद्रीनाथ धाम में बारह वर्ष तक तप कर अपनी चुम्बकत्व-शक्ति को अत्यधिक उत्कृष्ट बना लिया था। तभी उन्हें प्रद्युम्न के रूप में मनोवांछित सन्तान प्राप्त हो सकी थी। वैज्ञानिकों का मत है कि जीन्स की विशेषताएं विकिरणों द्वारा प्रभावित की जा सकती हैं। शरीर के भीतर रश्मियों के केन्द्रीयकरण द्वारा ऐसी विकिरण-चिकित्सा व्यवस्था की जा सकती है। विद्युत-क्षेत्र (इलेक्ट्रिक-फील्ड्स) द्वारा जीन्स की रासायनिक और विद्युतीय दोनों विशेषताओं में परिमार्जन संशोधन किये जा सकते हैं। ध्वनियों तथा अतिध्वनियों के क्षेत्र में भी खोजें चल रही हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि उनके द्वारा भी जीन्स में परिवर्तन की विधि खोजी जा सकती है।
भौतिक विज्ञान से यह सम्भव हो या न हो, पर अध्यात्म विज्ञान से तो यह साध्य है ही। भारतवर्ष में साधना द्वारा शरीरस्थ जैवीय विद्युत को प्रखर बना कर मन्त्रों के माध्यम से उत्पन्न अतिध्वनियों तथा यज्ञादि के विकिरण का उपयोग इस दिशा में सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। इन्द्र को जीतने में समर्थ वृत्रासुर की उत्पत्ति तथा राजा दशरथ के यहां राम भरत जैसी सुसन्तति की प्राप्ति ऐसे ही प्रयोगों द्वारा सम्भव हुई थी।
अध्यात्म विज्ञान वहां से आरम्भ होता है जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं प्रायः समाप्त हो जाती हैं। स्थूल की अगली सीढ़ी सूक्ष्म है। अन्तःस्रावी ग्रन्थियों से निकलने वाले विचित्र हारमोन स्रावों की तरह आनुवंशिकी क्षेत्र के रहस्यमय घटक ‘जीन’ भी उतने ही विलक्षण हैं। इन्हें प्रभावित करने में, भौतिकी सफल न हो सके तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। सुनियोजित अध्यात्म विज्ञान के पीछे वे सम्भावनाएं झांकती हैं जिससे न केवल हारमोन और जीन वरन् ऐसे-ऐसे अनेकों रहस्यमय केन्द्र प्रभावित परिष्कृत किये जा सकते हैं जो सामान्य मनुष्य जीवन को असामान्य—देवोपम बना सकने में समर्थ हैं। अध्यात्म विज्ञान की ‘अन्नमय कोश’ की कक्षा-प्रयोग प्रक्रिया इसी उद्देश्य को पूरा करती है।
अन्नमय कोश के सूक्ष्म घटक
अन्नमय कोश के बाह्यावरण से आगे चलकर इसका अध्ययन किया जाय तो इसका स्वरूप सूक्ष्म क्षमताओं से भरा हुआ उभर कर सामने आयेगा किसी भी क्षेत्र में उच्चस्तरीय साधक का सारा शरीर उसकी मुख्य साधना में सहयोगी बन जाता है। श्रेष्ठ चित्रकार जब किसी चित्र की कल्पना करता है तो इसके शरीर की हर इकाई इसके स्पंदनों से प्रभावित होती है। शरीर की हलचल में उस कल्पना के स्पंदन समाविष्य हो जाते हैं तथा निर्जीव तूलिका सामान्य रंगों में ही जीवंत चित्र का निर्माण कर देती है। वाणी के साधक गायक के मन में जो भाव उभरते हैं वह उसके हाव-भाव तथा स्वर लहरी में न जाने कहां से—कैसे गुंथ जाते हैं और उसमें अद्भुत प्रभाव पैदा कर देते हैं। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान चिकित्सक के चर्मचक्षुओं और मांस-पेशियों में न जाने क्या विशेषता आ जाती है कि वह रोग के सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह तथा गम्भीर से गम्भीर स्तर को पकड़ लेता है। इन साधकों के चमत्कारों के पीछे यही तथ्य छिपा है कि उनके अन्नमय कोश की हर इकाई उनके अन्दर की सूक्ष्म सम्वेदनाओं को अनुभव करने, स्वीकार करने तथा उसके अनुरूप प्रभाव पैदा करने में सक्षम हो जाती है। उसके संस्कार उसके अनुरूप हो जाते हैं। किसी भी उच्चस्तरीय साधना के लिये विज्ञान से लेकर उपासना तक के लिये अपने अन्नमय कोश को ऐसी ही सुसंस्कृत, सुयोग्य, सक्षम स्थिति में लाना आवश्यक होता है। उसके लिये उसकी मूल इकाइयों को विशेष रूप से गढ़ना-ढालना पड़ता है। इसे ही अन्नमय कोश का परिष्कार विकास की साधना कहा जाता है।
प्रश्न उठता है कि क्या अन्नमय कोश की मूल इकाइयों को वांछित ढंग का बनाया जा सकता है? हां, यह सम्भव है। इसकी पुष्टि भारतीय दर्शन की सनातन मान्यता तथा वर्तमान वैज्ञानिक शोधों, दोनों ही आधारों पर होती है। वस्त्र आदि तो जैसे बन गये वैसे बन गये कैनवास को मखमल में नहीं बदला जा सकता। क्योंकि वह जड़ संस्थान है। किन्तु शरीर तो चेतन संस्थान है। उसमें नये कोशों का निर्माण तथा पुरानों का विघटन सम्भव ही नहीं है, वह तो उसकी एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धीमी पड़ने से ही मनुष्य शरीर जराजीर्ण होने लगता है। जरा बुढ़ापा कुछ और नहीं अन्नमय कोश में नवीन स्वस्थ कोशिकाओं की संरचना तथा पुरानों के निष्कासन की गति शिथिल हो जाना मात्र है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित, नियमित बनाकर शरीर संस्थान में क्रमशः इच्छित परिवर्तन लाये जा सकते हैं।
सामान्य व्यक्तियों में भी अन्नमय कोश की इकाइयों में परिवर्तन होता ही रहता है। किन्तु उसकी कोई व्यवस्था, योजना न होने के कारण एक ढर्रा भर चलता रहता है। सामान्य रूप से किसी भी फैक्ट्री में पुराने पुर्जों तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर नये पुर्जे एवं नई मशीनों को स्थापित करने का क्रम चलता ही रहता है। उससे एक ढर्रे का उत्पादन निकलता भी रहता है। किन्तु कोई कुशल शिल्पी-उद्योगी जब अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाने, नयी वस्तुएं उत्पादित करने की योजना बनाता है तो फिर ढर्रे का क्रम पर्याप्त नहीं। उस स्थिति में लक्ष्य को ध्यान में रखकर सूझबूझ के साथ हर परिवर्तन व्यवस्थित ढंग से करना होता है। पुर्जों और मशीनों से लेकर औजार (टूल) तथा कच्चे माल की व्यवस्था भी उसी योजना के अनुरूप करनी होती है। अपने शरीर की हर कोशिका को एक सजीव पुर्जा, औजार, मशीन मानकर उन्हें लक्ष्य के अनुरूप बनाना, उसके लिये उपयुक्त आहार विहार अपनाना, योग साधक के लिये आवश्यक हो जाता है।
सामान्य व्यक्ति के अन्नमय कोश तथा योगी के अन्नमय कोश में अन्तर क्यों? किस आधार पर आवश्यक है? इसे एक सामान्य उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बिजली की लाइन को लें। विद्युत तारों में बहती है। उन्हें सहारा देने के लिये खम्भे रहते हैं। तार और खम्भों के बीच में ऐसे उपकरण लगे रहते हैं जो बिजली को खम्भों में होकर पृथ्वी में प्रविष्ट होने से रोके रहें। उन्हें ‘कुचालक इन्सुलेटर’ सामान्य दबाव (वोल्टेज) की विद्युत के लिये तार खम्भे तथा इन्सुलेटर सामान्य ही चल जाते हैं। किन्तु यदि ऊंचे दबाव (हाईवोल्टेज) की बिजली अधिक मात्रा में प्रवाहित करनी हो तो उसके लिए यह सभी उपकरण विशिष्ट स्तर के लगाने पड़ते हैं। यही बात सामान्य व्यक्ति तथा विशिष्ट साधक के साथ लागू होती है। सामान्य जीवनक्रम में सामान्य शारीरिक जैवीय विद्युत (बायो इलेक्ट्रिसिटी) की ही आवश्यकता पड़ती है, किन्तु उच्च लक्ष्यों के लिये अधिक प्रखर शक्ति तरंगें पैदा करनी होती हैं। उनका सम्वेदन, संचार करने के लिये अधिक सशक्त संस्थान की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़नी ही चाहिये। इसीलिये साधक को अपने अन्नमय कोश के परिष्कार, उसकी पुष्टि और विकास के लिए विशेष ध्यान देना, विशेष प्रयास करना होता है। तभी वह प्राणमय मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोशों के विकास में सहायक बनने तथा उनकी विकसित स्थिति के साथ तेलमेल बिठाने में समर्थ हो पाता है।
ताल-मेल बिठाने की बात यों ही नहीं कही गई है, उसका अपना विशिष्ट अर्थ है। निर्जीव घटक तालमेल नहीं बिठा सकते, वह तो चेतना सम्पन्न के लिए ही सम्भव है। अन्नकोश की हर इकाई, हर कोशिका (सैल) को आज के वैज्ञानिक भी स्वतन्त्र जैविक इकाई मानने लगे हैं। हर सैल में उसका हृदय न्यूक्लियस होता है। उसके श्वांस संस्थान को वैज्ञानिक भाषा में ‘माइटो कौंकिया’ कहते हैं। हर सैल में एक ‘गाल्गी एप्रेटस’ होता है जो उनके पाचन संस्थान का काम करता है। हर कोश अपने जैसे नये कोश का उत्पादन कर सकता है। इस व्यवस्था को वैज्ञानिक ‘न्यूक्लियोलस एण्ड क्रोमेटिन नैटवर्क’ कहते हैं। हर सैल में अपनी एक विशिष्ट जैवीय विद्युत का प्रभार (चार्ज) होती है जिसे उसका प्राण कहते हैं। इस प्रकार हर कोशिका एक स्वतन्त्र जैविक इकाई के रूप में अपने अस्तित्व को बनाये रखते हुए, शरीर संस्थान से अपना तालमेल बिठाये रखता है।
अन्नमय कोश के कोटि-कोटि सदस्य यह कोशिकाएं (सैल) इस उद्देश्य-लक्ष्य के अनुरूप स्वयं में स्वाभाविक क्षमता उत्पन्न कर सकें, उसके लिये विशिष्ट संस्कारवान नयी कोशिकाओं का उत्पादन कर सकें, तो उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति की सुनिश्चित पृष्ठभूमि बन जाती है। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से—योजनाबद्ध प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। उनके लिये आहार, विहार, चिन्तन आदि की विशिष्ट एवं व्यवस्थित पद्धति का अनुकरण करना होता है। जैसे बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए उन्हें साधन ही नहीं श्रेष्ठ संस्कार भी देने पड़ते हैं, इसी प्रकार इन कोशिकाओं के लिए भी आहार व्यवहार से लेकर ध्यान उपासना तक के अनेक माध्यम अपनाने होते हैं। उन सबके संयोग से ही अन्नमय कोश की प्रभावशाली साधना का स्वरूप बनता है।