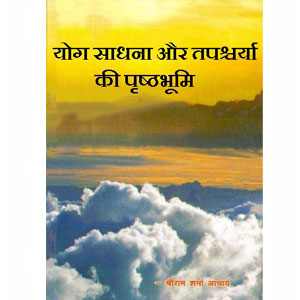योग साधना और तपश्चर्या की पृष्ठभूमि 
तपश्चर्या का तत्व ज्ञान
Read Scan Versionब्रह्म विद्या के—अध्यात्म विज्ञान के दो भाग हैं—एक आस्था पक्ष दूसरा क्रिया पक्ष। आस्था पक्ष में चिन्तन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले समस्त ज्ञान विस्तार को सम्पिलित किया गया है। वेद शास्त्र, उपनिषद्, दर्शन, नीतिशास्त्र आदि इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए रचे गये हैं। पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का—कथा प्रवचनों का—माहात्म्य इसी आधार पर बताया गया है कि उस प्रक्रिया के सहारे मानवी चिन्तन का परिष्कार होता रहे। अवांछनीय पशु-प्रवृत्तियों के कुसंस्कार छुड़ाने में, यह ज्ञानसाधना साबुन का काम करती है। विकृत मनोवृत्तियों से छुटकारा मिलता है और विवेक युक्त दूर दर्शिता का पथ-प्रशस्त होता है। प्रज्ञा, भूमा, ऋतम्भरा इसी परिष्कृत चिन्तन का नाम है। ‘ज्ञानमुक्ति’ ‘नहिं ज्ञानेन सदृश पवित्र मिह विद्यते’ जैसी उक्तियों में सद्ज्ञान को अध्यात्म का प्राण माना गया है। वेदान्त दर्शन को तो विशुद्ध रूप से ज्ञान साधना ही कहा जा सकता है। इसी सद्ज्ञान संवर्धन की बहुमुखी प्रक्रिया को अध्यात्म विज्ञान में ‘योग’ नाम दिया गया है।
अध्यात्म विज्ञान का दूसरा पक्ष क्रिया परक है—इसे ‘तप’ कहते हैं। आत्म निर्माण इसका एक चरण है और लोक कल्याण दूसरा। इन दोनों के लिए जो भी प्रयत्न करने पड़ते हैं, उनमें अभ्यस्त पशु-प्रवृत्तियों को चोट पहुंचती है। स्वार्थ साधनों में कमी आती है—और परमार्थ प्रयोजनों की सेवा साधना करते हुए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वार्थ सुविधा में कटौती करके ही परमार्थ की दिशा में कुछ किया जा सकता है। प्रत्यक्षतः यह सांसारिक दृष्टि से घाटे का सौदा है और अभ्यस्त प्रवृत्ति से विपरीत पड़ने के कारण कष्टमय, भी अनुभव होता है, इन कठिनाइयों को पार करने के लिए शरीर की तितीक्षा का, मन की सादगी का तथा इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का, सामना करने योग्य आन्तरिक साहसिकता का सहारा लेना पड़ता है। अपने आपे को इसी ढांचे में ढालने के लिये, जितने भी प्रयास किये जाते हैं, वे सब ‘तप’ की श्रेणी में गिने जाते हैं। यदि आस्थाओं का स्तर बदला जा सके और मात्र चित्र-विचित्र शारीरिक क्रियायें करते रहा जाय, तो इतने भर का प्रभाव शरीर तक ही सीमित रह जायेगा। चेतना का वह परिष्कार न हो सकेगा जो तपश्चर्या का मूलभूत उद्देश्य है।
आत्मिक प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिये योग और तप के दोनों कदम बढ़ाते हुए, लेफ्ट राइट की परेड करते हुए, गतिशील होना पड़ता है। ज्ञान और विज्ञान की दोनों धाराएं, गंगा यमुना की तरह जब मिलती हैं, तब प्रभु प्राप्ति का संगम—सुअवसर हाथ में आता है। भिन्न-भिन्न परम्पराओं में अपनी ज्ञान साधना और कर्मकाण्ड प्रक्रिया को कई तरह से निर्धारित किया है, पर सभी का मूल प्रयोजन समान है। मानवी सत्ता भी चेतन आत्मा और जड़ शरीर के समन्वय से बनी है। उन दोनों को ही परिष्कृत करना पड़ता है। भाव शुद्धि की तरह क्रिया शुद्धि भी आवश्यक है। भाव शुद्धि को योग तथा क्रिया शुद्धि को तप कहा जाता है।
मन, चेतन-आत्मा और जड़-शरीर का मध्यवर्ती है। इसे दोनों की सम्मिलित सत्ता कहा जाता है इसे चेतन होते हुए भी ग्यारहवीं इन्द्रिय माना गया है। इससे स्पष्ट है कि वह चेतन होते हुए भी जड़ की ओर आकर्षित बना रहता है। दोनों क्षेत्रों से सम्बन्धित होने के कारण मन को ही चेतना और काया के परिष्कार की भूमिका निभानी पड़ती है, आखिर गिराने का कारण भी तो वही है।
मन की दो विशेषताएं सर्व विदित हैं—(1) चंचलता (2) सुख लिप्सा। उसे आवारा लड़कों की तरह मटरगश्ती में मजा आता है। बन्दरों की तरह डाली-डाली पर उछलते रहने और चिड़ियों की तरह जहां-तहां फुदकते रहने में उसकी चंचलता को समाधान मिलता है। कल्पना के घोड़े पर सवार होकर वह आकाश-पाताल की सैर करता है। इस भटकाव में उसकी अधिकांश शक्ति नष्ट हो जाती है। इसे रोककर उपयोगी लक्ष्य पर उसे केन्द्रित करने का प्रयास योगाभ्यास कहलाता है। योग के फलस्वरूप भौतिक जीवन में दरिद्रता का समृद्धि में लय हो जाता है। पिछड़ापन प्रगतिशीलता में परिणत हुआ दीखता है। विभिन्न प्रकार की सांसारिक सफलताएं मन को लक्ष्य विशेष पर केन्द्रित करने का ही सत्परिणाम है। उसी से प्रबल पुरुषार्थ बन पड़ता है। अभीष्ट साधन जुटते जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां बनती जाती हैं।
आत्मिक क्षेत्र में मन को लगा देने से प्रसुप्त शक्ति संस्थानों के जागरण का वातावरण बनता है और दिव्य क्षमताएं प्रकाश में आती हैं। यह आन्तरिक प्रगति सामान्य व्यक्ति को महामानव स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देती है। यह सब मन के भटकाव को रोकने और उसे लक्ष्य केन्द्र पर नियोजित कर सकने का ही प्रतिफल है। चंचलता की वृत्ति से छुटकारा पाकर एकाग्रता के लिए—एक धारा में बहने के लिए सधाया हुआ मन कितने चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करता है इसे अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रगति का समूचा इतिहास तो इस तथ्य का साक्षी है ही।
मन की दूसरी प्रवृत्ति है—सुखोपभोग की लिप्सा। भौतिक सुख शरीर द्वारा वासना तृप्ति के रूप में भोगा जाता है। इन्द्रियां इसकी माध्यम हैं। शिश्नोदर परायणता में रुचि बनी रहती है। स्वाद और विषय सुख की कल्पनाएं करने और साधन जुटाने के ताने-बाने बुनने में उसकी अधिकांश शक्ति लगी रहती है। मधुर देखने, सुनने, सूंघने छूने आदि की इन्द्रिय लिप्साएं भी इसी विलास क्षेत्र में आती हैं। अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरों को प्रभावित करने वाले कई तरह के ठाट-बाट बनाये जाते हैं। संग्रह और स्वामित्व के लिए भी अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। ‘तृष्णा’ शब्द में इन सबका समावेश है। अहंता पर चोट पहुंचने से प्रतिशोध की उत्तेजना उत्पन्न होती है। यह क्रोध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यह छह आन्तरिक शत्रु माने गये हैं। संक्षेप में यह सारा विकार परिवार भौतिक सुख प्राप्त करने की मनः लिप्सा की अनेकों रंग रूपों में दीखने वाली प्रतिक्रियाएं मात्र हैं।
मन की इस पतनोन्मुख बहिर्मुखी-लिप्सा परायण प्रवृत्ति से जीवात्मा को असीम हानि उठानी पड़ती है। जीवन सम्पदा उन्हीं उलझनों में नष्ट-भ्रष्ट होती चली जाती है और इस सुरदुर्लभ अवसर का समुचित लाभ उठाने से वंचित रहना पड़ता है।
मन की इस प्रवृत्ति को उलट देने के लिए किये गये प्रयास ‘तप’ कहलाते हैं। सुखानुभूति तो आत्मा की आकांक्षा भी है, पर वह मन के स्तर से बहुत ऊंची, बहुत भिन्न है। मन की तृप्ति वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति में होती है। इसमें उपभोग लक्ष्य है। आत्मा उच्चस्तरीय आदर्शों के पालन में जो आनन्द पाता है, उसे सन्तोष या शान्ति कहते हैं। संक्षेप में मन को भौतिक सुख की आकांक्षा रहती है और आत्मा को आत्मिक सन्तोष एवं शान्ति की। सुख मन का विषय है और सन्तोष आत्मा का। रस्साकशी में एक को हारना दूसरे को जीतना पड़ता है। मन जीतता है तो आत्मा को असहाय बनकर अतृप्त स्थिति में पड़ा रहना होता है। आत्मा जीतता है तो मन को कुचलना पड़ता है। आरम्भ में उद्धत मन को संयम बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। पीछे तो उनमें समझौता हो जाता है। वन्य पशु जब पालतू बन जाते हैं तो मालिक से झगड़ने की अपेक्षा उसी के साथ फिरने लगते हैं। यही स्थिति मन की होती है। साधना द्वारा मन को इसी तरह सधाया जाता है, जिस प्रकार सरकस वाले सिंह जैसे आक्रमणकारी जन्तु को स्वामिभक्त, आज्ञाकारी एवं उत्पादक बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सरकस के पशु शिक्षक उन जन्तुओं की अनगढ़ आदतों को छुड़ाने और नये प्रकार के अभ्यास डालने में भारी माथापच्ची करते हैं। उन्हें मार और प्यार की दुहरी भूमिका निभानी पड़ती है। तप साधना और कुछ नहीं। मन की चंचलता और सुख लिप्सा वाली अनगढ़ आदतों को छुड़ाने और उसे उपयोगी प्रवृत्तियों में संलग्न होने का अभ्यस्त बनाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें मोटेतौर से क्रूरकर्मा की संज्ञा भी दी जा सकती है। तप का बाह्य स्वरूप कुछ ऐसा ही निष्ठुरतापूर्ण है, यद्यपि आत्मोत्कर्षण का उसके पीछे दूरगामी दुलार ही दुलार छलकता देखा जा सकता है।
सुख को गौण और सन्तोष को प्रधान मानकर चलना—मन को गौण और आत्मा को प्रधान मानना यही वह परिवर्तन है जिसके आधार पर किसी को तपस्वी कहा जा सकता है। तप में तितीक्षा का—शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक असुविधाओं का अभ्यास इस लिए करना पड़ता है कि मन की अनगढ़ कुसंस्कारिता को—चंचलता और लिप्सा को छुड़ाया जा सके। उसे पतनोन्मुखी बहिरंग ललकों से विरत करके उच्चस्तरीय आध्यात्मिक आदर्शवादिता अपनाने के लिए सहमत करना ही तप साधना का एकमात्र उद्देश्य है। इसमें जो कड़ाई बरतनी पड़ती है उसे सुधार प्रयोजन के लिए कुछ क्षण के लिए बरती गई विवशता भर समझा जाना चाहिए। उसे प्रसव पीड़ा की उपमा दी जा सकती है। ऐसे तो सत्परिणाम प्राप्त करने के लिए किसान, विद्यार्थी, पहलवान, श्रमिक, व्यवसायी, कलाकार आदि को बाल चंचलता से विरत होने के लिए मन मारना पड़ता है और अपने रूखे नीरस प्रयोजनों में तन्मय होना पड़ता है। मोटेतौर से इस साधना को अपने साथ बरती गई कठोरता ही कह सकते हैं। दूसरे शौक-मौज में निरत साथी इसी मूर्खता भी कह सकते हैं, पर वस्तुतः वह आरम्भ में बीज की तरह गलने के लिए और पीछे विशाल वृक्ष के रूप में विकसित करने वाली दूरगामी बुद्धिमत्ता ही है।
तपस्वी को आरम्भ में कष्ट सहना पड़ता है। उसकी शारीरिक सुख सुविधाओं में कटौती होती है, मानसिक हास-परिहास का अवसर भी छिनता है, औचित्य को रखकर उपार्जन और उदार उपयोग का ध्यान रखने से समृद्धि भी बढ़ नहीं पाती। इन तीनों क्षेत्रों में कमी पड़ने को मोटेतौर से मूर्खता कह सकते हैं, पर चूंकि उसके पीछे जो उज्ज्वल सम्भावनाएं विद्यमान हैं, उन्हें थोड़ी लागत में तगड़ा मुनाफा कमाने जैसी बुद्धिमत्ता ही कहा जा सकता है।
तपाने से वस्तुएं गरम होती हैं और उनका संशोधन होता है, दृढ़ता आती है तथा स्तर बढ़ता है। वस्तुओं की तरह ही व्यक्ति भी तप-साधना से परिष्कृत होता और सुदृढ़ बनता है।
कच्ची मिट्टी से बनी ईंटों द्वारा विनिर्मित मकान वर्षा में गलने लगता है, पर यदि इन्हीं ईंटों को आग में पका लिया जाय तो उनसे बनी इमारतें मुद्दतों चलती हैं। चूना और सीमेंट क्या है? कंकड़ पत्थरों का पका हुआ चूरा। यदि इन्हें कच्चा पीसकर इमारत में लगाया जाय तो काम नहीं चलेगा। पकाये जाने पर उनमें ईंटों को पकड़ लेने और भवन को चिरस्थायी बना देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। धातुएं खदान में से मिट्टी मिली—कच्ची अवस्था में निकलती हैं। उन्हें भट्टी में तपाया जाता है तब लोहा, तांबा आदि शुद्ध बनते और काम में आते हैं। लोहे को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसे अधिक तपाया जाता है। काटने वाले शस्त्र तथा औजारों की ‘धार’ अधिक गर्मी देकर ही सुस्थिर बनाई जाती है।
आयुर्वेद के रसायनवेत्ता कई प्रकार की गुणकारी भस्में बनाते हैं। अभ्रक, भस्म वंग-भस्म, प्रबाल भस्म, लौह भस्म आदि के गुण प्रख्यात हैं। यह उन साधारण सी वस्तुओं के तपाने, गरमाने का ही प्रतिफल है। पानी गरम करने से भाप बनती है और उससे रेलगाड़ी का इंजन जैसी भारी वस्तुएं धकेली जाती हैं। बल्ब का जरा-सा ‘फिलामेट’ जब गरम होता है तो रोशनी देता है। दीपक के बारे में भी यही बात है, गर्मी ही प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है, उसी को शक्ति के रूप में परिणत किया जाता है। व्यक्तित्व की सत्ता को तपाने से भी उसमें सर्वतोमुखी प्रखरता उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को गुरुकुलों के कठोर वातावरण में रहकर बढ़ने के लिए भेजा जाता था कि वे कष्टसाध्य जीवनयापन करते हुये अपने शरीर को सुदृढ़ और मन को सहनशील बनाने की साधना में उत्तीर्ण होकर प्रखर प्रतिभा विकसित कर सकें।
कच्चे फलों को भूसे या अनाज की गर्मी में बन्द रख कर पकाया जाता है। आम प्रायः इसी प्रकार पाल में पकता है और अपना खट्टापन हटाकर मीठा बनता है। दूध को गरम करने पर घी उपलब्ध होता है। सामान्य पानी को औषधि उपयोगी डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए उसे भट्टी पर चढ़ाया जाता और भाप बनाकर उड़ाया जाता है। तप साधना द्वारा कष्टसाध्य परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें सहन करने की तितिक्षा का सहारा लेकर अपने को परिष्कृत करना पड़ता है, सोने को आग में तपाकर ही विविध प्रकार के आभूषण बनते हैं। अन्य धातुओं से भी उपकरण तभी बनते हैं जब उन्हें आग में डालकर कोमल बनाया जाय। मनुष्य की जड़ता एवं कठोरता को सुकोमलता में बदलने और अमुक ढांचे में ढालने के लिये तपश्चर्या की रीति-नीति अपनाना आवश्यक होता है। आरामतलबी और सुख-सुविधा से भरे वातावरण में पलने वाले लोग अविकसित स्थिति में पड़े रहते हैं उनकी विविध क्षमताएं विकसित होने की बात बनती ही नहीं। उस्तरे पर धार रखने से ही उसमें पैनापन बढ़ता है और चमक दीखती है। उसे ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहने दिया जाय तो धीरे-धीरे जंग चढ़ती जायगी और वह गल कर अपनी मौत मर जायगा। सुविधा के अभिलाषी लोग अपना पुरुषार्थ खोते चले जाते हैं। तीक्ष्णता की वृद्धि और रक्षा के लिए रगड़ आवश्यक है। फौज के सैनिकों को यदि नित्य ‘परेड’ करने और दौड़ लगाने का अवसर न मिले तो वे थोड़े ही दिनों में तोंद वाले सेट बन जायेंगे तब उनके लिये लड़ सकना तो दूर अपनी काया का बोझ ढोना भी कठिन पड़ेगा।
इतिहास, पुराणों में ऐसे असंख्य आख्यान मौजूद हैं जिनसे प्रतीत होता है कि विशिष्ट शक्ति सम्पन्न लोगों को विभूतियां उपार्जन में तप-साधना का ही आश्रय लेना पड़ा था। भगीरथ द्वारा तप करके गंगा को धरती पर लाया जाना, पार्वती का शिव से विवाह सम्पन्न होना, ध्रुव का तप करके ब्रह्माण्ड का केन्द्र बनना, दधीचि की अस्थियों से वज्र बनना और उससे असुरों का मारा जाना, अगस्त्य का समुद्र शोषण, विश्वामित्र का नई सृष्टि का निर्माण, सात सामान्य मनुष्यों का सप्त ऋषि बनना—जैसी अगणित कथाएं तप की शक्ति का परिचय प्रस्तुत करती हैं।
भगवान कृष्ण को सुसंतति प्राप्त करने के लिये रुक्मणी सहित लम्बी अवधि तक मात्र जंगली बेर खाकर उस स्थान पर तप करना पड़ा था, जहां आजकल बद्रीनाथ धाम है। दलीप ने रानी सहित वशिष्ठ की गाएं चराने का दीर्घकालीन तप करके सुसंतति प्राप्त की थी। स्वायंभु मनु और शतरूपा रानी के तप ने उन्हें राम जैसा पुत्र दिया था कश्यप तथा अदिति के तप ने कृष्ण को गोदी में खिलाने का वरदान दिलाया था। इन प्रसंगों में यह प्रतिपादन है कि तप द्वारा मनुष्य भगवान का भी पिता बन सकता है। आत्म-साधना में तपश्चर्या को प्रमुखता दी गई है। तप के कारण उसकी गर्मी से प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की परिस्थितियां बनती हैं। इसीलिए आत्मिक प्रगति की साधना में कई प्रकार के कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं। व्रत उपवास, ब्रह्मचर्य जैसी तितीक्षाओं से शरीर को इस योग्य बनाया जाता है कि वह कठिनाइयां सहने का अभ्यस्त तथा तज्जनित गर्मी से सुदृढ़ होने का अवसर प्राप्त कर सके।
उपवास के लाभ सर्वविदित हैं। पेट को विश्राम देने से उसमें जमा अपच दूर होता है और थकान दूर होने से पाचन क्रिया में तीव्रता आती है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रोग निवृत्ति का प्रधान उपाय उपवास को माना गया है। उदर शोधन के अतिरिक्त उपवास का विशेष लाभ यह है कि उससे मनोविकारों का शमन होने लगता है। जो शक्ति पाचन में लगती है वह यदि बच सके तो उसका उपयोग मन के अपच को—विचार विकृति को दूर करने में लग सकता है। भारतीय धर्म में पुण्य पर्वों एवं शुभ अवसरों पर उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। विवाह के दिन वर-वधू के उपवास करने की प्रथा है। दैनिक उपासना पूरी न हो जाने तक कुछ न खाने पीने का नियम कई लोग पालते हैं—यह उपवास का ही छोटा रूप है। उपवास को तप माना गया है।
अन्न का मन से घना सम्बन्ध है। दैनिक जीवन में सतोगुणी आहार ही अपनाने की बात ध्यान में रखी जाय तो उसका प्रतिफल विचार शुद्धि के रूप में भी परिलक्षित होगा। नीति उपार्जित परिश्रम की कमाई ही खाई जाय। पकाने वाले तथा परोसने वाले व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पवित्र हों। खाते समय भगवान को मन ही मन भोग लगाने और उसे प्रसाद समझ कर औषधि रूप में ग्रहण करने की भावना रखी जाय। चटोरेपन को विलासिता से बच कर केवल आहार की सात्विकता भर से संतुष्ट रहा जाय। अन्न को देवता मानकर उसका सम्मान किया जाय और जूठन के रूप में उसकी अनावश्यक बर्बादी न की जाय। यह बातें सामान्य लगती हैं, पर आत्मिक प्रगति की दृष्टि से उनका बहुत महत्व है। ‘‘जैसा खाये अन्न—वैसा बने मन’’ वाली उक्ति बहुत ही सारगर्भित है। मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। उसके लिए आहार शुद्धि को प्रथम चरण कहा जा सकता है। मांसाहार—नशेबाजी—अशुद्ध व्यक्ति और वातावरण में पकाया और परोसा गया मिर्च मसालों से भरा गरिष्ठ और उत्तेजक आहार मनःक्षेत्र में तमोगुण उत्पन्न करता है और उसका प्रभाव चित्त की अस्थिरता बनकर उपासना क्रम में भारी विघ्न उत्पन्न करता है।
पिप्पलाद ऋषि पीपल वृक्ष के फल खा कर निर्वाह करते थे। कणाद ऋषि शिलौञ्च वृत्ति से जंगली धान्य खाकर गुजारा करते थे। यह अन्न शुद्धि की प्रक्रिया है। हमें स्वयं लम्बी अवधि एक मात्र जौ की रोटी और छाछ इन दो ही वस्तुओं पर हर कर पुरश्चरण क्रम चलाना पड़ा है। अभक्ष्य खाने से मन की विकृति का होना स्पष्ट है। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह जब धर्मोपदेश दे रहे थे तप द्रोपदी ने पूछा—देव! जब मुझे भरी सभा में निर्वासन किया जा रहा था, तो आपने यही धर्मोपदेश कौरवों को क्यों नहीं दिये? उत्तर में भीष्म ने इतना ही कहा—उन दिनों में कुधान्य खा रहा था, अस्तु धर्मज्ञान रहते हुए भी उसे चरितार्थ करने का साहस सम्भव न हो सका।
आहार शुद्धि के लिए हम अपने खाद्य पदार्थों में सात्विक वस्तुएं ही स्वीकार करें। दो बार से अधिक भोजन न करने का नियम बनालें। दूध, छाछ, रस, क्वाथ जैसे पेय पदार्थों के अतिरिक्त बीच-बीच में अन्य चीजें न लें। भूख से कम खायें। जल्दी न निगलें, चबा कर खायें। सप्ताह में एक दिन अथवा एक जून निराहार रहें अथवा फल शाक दूध आदि पर निर्वाह करें। साप्ताहिक उपवास की परम्परा चल पड़े तो देश की जटिल खाद्य समस्या का सहज समाधान निकल सकता है। साथ ही अपच का हल निकल आने से स्वास्थ्य संकट भी बहुत हद तक हल हो सकता है।
सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत का पालन भी एक प्रकार का उपवास ही माना जा सकता है। नमक, मसाले, शकर जैसी वस्तुएं मात्र स्वाद के लिए खाई जाती हैं। उपयोगी स्तर का—उपयुक्त मात्रा में नमक शकर आदि तो अन्न, शाक, फल, दूध आदि में सहज ही मिल जाता है। ऊपर से इन चीजों का लिया जाना स्वास्थ्य के लिए नहीं वरन् स्वाद के लिए ही प्रयुक्त होता है। स्वाद के लोभ में आहार की अधिक मात्रा उदरस्थ होती है और अपच उत्पन्न करके तरह-तरह के रोगों को जन्म देती है। स्वाद पर काबू पाना भी एक प्रकार का तप है। बिना नमक, शकर, मसाले आदि का भोजन सप्ताह में एक दिन भी किया जाता रहे तो इससे स्वादेन्द्रिय पर नियन्त्रण करने की तपश्चर्या चल पड़ेगी। गांधी जी ने अपनी ‘सप्त महाव्रत’ पुस्तिका में ‘अस्वाद’ को प्रथम व्रत माना है और उसके फलस्वरूप ब्रह्मचर्य पालन तथा मनोनिग्रह में सफलता मिलने का प्रतिपादन किया है।
मनोनिग्रह तपश्चर्या में दूसरा व्रत ब्रह्मचर्य पालन है। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से रतिक्रिया के अवसर न्यूनतम ही आने देने चाहिए। बहुमूल्य जीवन रस को फुलझड़ी की तरह जलाने का अत्यन्त महंगा खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। इससे अपनी और सहयोगी की हानि ही हानि है। क्षणिक विनोद की तुच्छता और शक्ति संचय की महत्ता को समझते हुए इस दिशा में अधिकाधिक संयम बरता जाना ही दूरदर्शिता है। इस बचत का लाभ शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता के रूप में सामने आता है और आत्मिक प्रगति की दिशा में उस संचय से भारी सहायता मिलती है।
शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्व मानसिक कामुकता से बचने का है। शरीर क्षण तो यदा-कदा ही होता है, पर कुदृष्टि एवं काम चिन्तन के फलस्वरूप मानसिक विकृति घड़ी-घड़ी उत्पन्न होती रहती है। काम सेवन से जिस प्रकार शारीरिक शक्ति घटती है उसी प्रकार काम चिन्तन से मनोबल एवं आत्मबल घटता है इससे आत्म-शक्ति में कमी पड़ती जाती है। ऐसी दुर्बल मनःस्थिति में वे आधार नहीं बन पाते जिनसे आत्मोत्कर्ष की दिशा में आशाजनक प्रगति संभव होती है। पुरुषों को नारियों के प्रति और नारियों को पुरुषों के प्रति पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए। कामुक चिन्तन भी मानसिक व्यभिचार माना गया है और उससे होने वाली हानि को आत्मिक प्रगति के मार्ग में भारी व्यवधान माना गया है। मन को कामुक चिन्तन से बचाने के लिए उसके प्रति-पक्षी पवित्र भावों को अधिक समय तक मन में स्थान देना चाहिए। जितनी देर अशुद्ध चिन्तन के लिए मस्तिष्क को छूट दी जाती है, उतनी ही सुविधा यदि परिष्कृत चिन्तन के लिए दी जा सके तो उस परिष्कृत मनोभूमि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, चिन्ता, निराशा, भय आदि का कोई कुविचार, मनोविकार पनप न सकेगा। सृजनात्मक शुभ चिन्तन के विचारों से मन को भरा पूरा रखने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिन्तन का आश्रय लेकर मनोभूमि ऐसी प्रौढ़, परिपक्व बनाई जा सकती है जिसमें कुविचारों को पैर जमाने के लिए तनिक भी गुंजाइश न रहे।
हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, समर्थ, विवेकानन्द आदि ब्रह्मचारियों के उज्ज्वल चरित्रों पर बार-बार विचार किया जाना चाहिए। शिवाजी ने एक अनिंद्य सुन्दरी को उपभोग के लिए प्रस्तुत किये जाने पर इतना ही कहा था—‘‘ऐसी सुन्दर मेरी माता होती तो मैं भी इतना सुन्दर होता’’। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन से उसी जैसा पुत्र पाने के उद्देश्य से काम प्रस्ताव किया तो अर्जुन ने उत्तर दिया—‘‘आप कुन्ती की तरह मेरी माता और मैं आपका सगे पुत्र की तरह बालक हूं। इसी प्रकार तत्काल आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है।’’ ऐसी ही पवित्र दृष्टि रखने से आत्मबल संचित होता है। इस मनोनिग्रह को तप की ही संज्ञा दी गई है। स्वादेन्द्रिय और कामेन्द्रिय की स्थूल और सूक्ष्म लिप्सा पर काबू पाया जा सके तो समझना चाहिए कि इन्द्रिय निग्रह का उद्देश्य पूरा हो गया। आंख, नाक, कान आदि की चित्त को चंचल बनाने में तनिक सी भूमिका रहती है। प्रधान तो यही दो स्वादेन्द्रियां हैं इनका उपभोग और चिन्तन रोकने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, उन सभी को तपश्चर्या का अंग माना गया है।
भूलों के लिये शारीरिक-मानसिक दण्ड प्रताड़ना को प्रायश्चित कहते हैं। यह भी तप वर्ग में ही आती हैं। दैनिक भूलों को समझना और भविष्य में ऐसा न होने देने की सतर्कता तीव्र करना—यदि नैतिक गलतियां हुई हैं तो उनके लिए भोजन में आंशिक कटौती, अमुक समय का मौन, नींद में कटौती, अतिरिक्त श्रम, उठक-बैठक जैसी प्रताड़ना, दण्ड व्यवस्था स्वयं की जा सकती है। पिछले जीवन में कोई बड़े अपराध बने हों, तो उनके लिए चांद्रायण व्रत, दाढ़ी बढ़ाना, अमुक समय तक नंगे पैर रहना, पैदल तीर्थ यात्रा, धन दान जैसी किन्हीं विशेष प्रायश्चित्यों की व्यवस्था किसी उपयुक्त नीतिवेत्ता के परामर्श से करनी चाहिए इससे मन पर चढ़े हुए पाप भार से निवृत्ति मिलती है।
स्थूल शरीर को तपाने वाली उपरोक्त कुछ कष्ट साध्य तप तितीक्षाओं का उल्लेख किया गया है। सूक्ष्म शरीर मन को तपाने के लिए तृष्णा और वासना का लोभ और मोह का परित्याग करना पड़ता है। वैराग्य इसी का नाम है। सादा जीवन उच्च विचार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सूक्ष्म शरीर में उत्कृष्टता बनी रहे इसके लिए सादगी का नम्रता एवं मितव्ययिता का अपनाया जाना आवश्यक है। खर्चीली तड़क-भड़क और उद्धत ठाट बाट से बचा जाय और भोजन, वस्त्र निवास आदि जीवनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में औसत नागरिक जैसी सादगी बरती जाय। खर्च उतना ही किया जाय जितना निर्वाह के लिए नितान्त आवश्यक हो। आवश्यकताएं और भौतिक महत्वाकांक्षाएं घटाई जायं ताकि उनमें लगने वाला समय श्रम और मनोयोग परमार्थ प्रयोजनों में लगाने के लिए बचाया जा सके।
(1) संयम और सादगी की नीति अपना कर शक्तियों के संचय एवं अभिवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहने में अपने साथ कठोरता बरतना (2) लोक मंगल के पुण्य प्रयोजनों में अपनी सामर्थ्य का बड़ा भाग लगाने के कारण स्वयं को कठिनाई में रहने की स्थिति का अभ्यास (3) स्वार्थरत लोगों जितना भौतिक लाभ उपार्जन करने में न्यूनता रह जाने पर भी सन्तोष (4) अनीति से संघर्ष करने में आसुरी तत्वों के आक्रमण से आघात। यह सब कारण ऐसे हैं जिनसे उच्चस्तरीय महा मानवोचित जीवन जीने वालों का आये दिन वास्ता पड़ता है। विलासी और महत्वाकांक्षी रीति-नीति अपनाने वालों का न्यायोचित उपार्जन अपनी बढ़ी-चढ़ी आवश्यकताएं भू पूरी नहीं कर पाता फिर वे मानवता के महान् कर्तव्यों का पालन करने के लिए समय और साधन कहां से पायें? यह प्रयोजन अपने साथ मितव्ययिता, कष्ट सहिष्णुता, मनोनिग्रह जैसी सख्ती बरते बिना और किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता।
अनीति पर उतारू लोगों को सिद्धान्तवादी सहन नहीं हो सकते। वे देखते हैं कि प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से वे उनके स्वेच्छाचार में बाधक हैं। नीति का समर्थन और अनीति का विरोध करना भी उनके स्वार्थों पर चोट पहुंचाता है। वे सोचते हैं, यह रोड़ा रास्ते से हटाकर निष्कंटक होना चाहिए। ऐसी दशा में अनीति पोषकों के आक्रमण का शिकार होना पड़ता है। फिर कई बार ऐसी विवशता आ जाती है कि अवांछनीयताओं को चुपचाप सहने के लिए अपना अन्तरात्मा तैयार नहीं होता और अन्याय से जूझने में बड़ी से बड़ी हानि उठाने के लिए भी अपना शौर्य-साहस तन कर खड़ा हो जाता है। प्रसिद्ध है कि आक्रान्ता लोग संगठित हमला करते हैं, पर बचाव पक्ष के लोग अपनी भीरुता अथवा तथाकथित शान्ति प्रियता के कारण मुंह छिपाये बैठे रहते हैं। चार गुण्डों का मुकाबला करने में चालीस सामान्य लोग हलके पड़ते हैं। ऐसी दशा में अन्याय विरोधी अकेला पड़ जाता है और उसे अपनी विरोधात्मक साहसिकता के कारण कई प्रकार के आघात सहने पड़ते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर सन्तों, सुधारकों और शहीदों को दुष्टों द्वारा तरह-तरह से सताये जाने के अगणित घटनाक्रम मिलते हैं। इनका दोष इतना ही था कि उनने अवांछनीयताओं के साथ असहयोग, विरोध प्रकट किया था और उनका उन्मूलन करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध न करने से अनीति को प्रोत्साहन मिलता है और वह सौ गुने उत्साह से विनाश पर उतारू होती है ऐसी दशा में प्रतिरोध अनिवार्य हो जाता है। तब जो इतना साहस दिखायें वे चोट सहने को भी तैयार रहें। इसी की पूर्व तैयारी के लिए भी कष्ट सहिष्णुता का पूर्वाभ्यास करना पड़ता है।
सुविधा भरा जीवन आलसी बनाता है और प्रतिभा को प्रसुप्त स्थिति में धकेल देता है। संघर्षमय, कठिनाई भरे जीवन में अन्य असुविधाएं कितनी ही क्यों न हों, इतना लाभ स्पष्ट है कि उससे मनुष्य की प्रखरता निखरती है। अमीरी के वातावरण में से कदाचित ही कभी कोई प्रतिभाएं उभरती हैं। संसार भर के महामानवों के इतिहास में यह तथ्य स्पष्ट है कि वे या तो कठिनाइयों की परिस्थिति में जन्मे थे अथवा उनने जान-बूझकर कठिनाइयों से भरा जीवन-क्रम अपनाया था। पत्थर पर रगड़ने से ही चाकू की धार तेज होती है। मानवी प्रतिभा के तीक्ष्ण होने में भी यही तथ्य काम करता है।
गायत्री पुरश्चरणों के समय आमतौर से साधकों को भोजन संयम, अस्वाद, व्रत-उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अपने शरीर की सेवा—कपड़े धोना, हजामत बनाना आदि कार्य स्वयं करना कोमल शैया त्याग कर भूमि या तख्त पर सोना, मारे हुए पशुओं का चमड़ा प्रयोग में न लाकर करुणा का परिचय देना, कुछ समय मौन रहना जैसी तितीक्षाएं बरतने के लिए कहा जाता है। इस निर्देश के पीछे तथ्य इतना ही है कि कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास करते हुए हर घड़ी यह विचार करते रहा जाय कि आदर्श जीवन जीने वाले के लिए स्वेच्छापूर्वक असुविधाएं सहन करने में उत्साह एवं सन्तोष करने का स्वभाव परिपक्व करना आवश्यक है। अभ्यास रहने से, वैसा चिन्तन चलते रहने से अवसर आने पर वे अड़चनें अप्रत्याशित नहीं लगतीं और सोचा जाता है यह तो होना ही था, इसकी तैयारी तो पूर्वाभ्यास के रूप में देर से की जाती रही है।
तप तितीक्षा में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाई को स्वेच्छापूर्वक आमन्त्रित किया जाता है। इसे देवता के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शन का प्रमाण माना जाता है। वस्तुतः यह देवता और कोई नहीं ‘आत्म देव’ ही है। अपने आपको परिष्कृत करके देव के स्तर तक पहुंचाने के प्रयास ही वास्तविक साधनाएं हैं। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तप साधन—विधान का ढांचा खड़ा किया गया है।
विज्ञान पक्ष की साधना में तपश्चर्या को केन्द्र मान कर चलने वाले विधि-विधानों का उद्देश्य है—प्रसुप्ति से निवृत्ति—मूर्छना से मुक्ति। इसके लिए गर्मी उत्पन्न करनी पड़ती है। गर्मी पाकर प्रसुप्ति से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय की वेला निकट आने पर प्राणियों की निद्रा टूटती है और वे जागते उठते एवं कार्यरत होते हैं। रात्रि में कलियां सिकुड़ी पड़ी रहती हैं पर जैसे ही सूर्य निकलता है वे हंसने खिलने लगती हैं। मानवी सत्ता के अन्तर्गत बहुत कुछ है। अत्युक्ति न समझी जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि सब कुछ है किन्तु है वह मूर्छित। इस मूर्छना के जगाने के लिए धूप, आग बिजली आदि से उत्पन्न बाहरी गर्मी से काम नहीं चलता। उसका प्रभाव भौतिक जगत में ही अपनी हल-चल उत्पन्न कर के रह जाता है। चेतना पर चढ़ी हुई मूर्छा को हटाने के लिए तप करना पड़ता है। उसके लिए भीतरी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। इसे कैसे उगाया और बढ़ाया जा सकता है, इसी विज्ञान को अध्यात्म की भाषा में तप कहते हैं।
तप की स्थूल प्रक्रिया सांकेतिक विधि वह है जिससे शरीर की स्वाभाविक सुख सुविधा को—वासना को रोका जाता है और मन की स्वाभाविक चंचलता को—अहंता और लोलुपता को प्रतिबन्धित किया जाता है। मनोनिग्रह इसी का नाम है। निरोध से शक्ति उत्पन्न होती है, खुले मुंह की पतीली में खौलता हुआ पानी भाप बनकर उड़ता रहता है और उसके तिरोहित होने में कोई अचंभे जैसी बात मालूम नहीं पड़ती, पर जब उसी को कड़े ढ़क्कन में बन्द कर दिया जाय तो फैली हुई भाप उस बर्तन को फाड़ कर भयंकर विस्फोट कर सकती है। स्टोव और प्रेशर कुकर फटने से दुर्घटना इसी निरोध का परिणाम होती हैं। इन्द्रियनिग्रह और मनोनिग्रह का महात्म्य इसी आधार पर बताया जाता है। ब्रह्मचर्य की महत्ता का रहस्य यही है कि ‘ओजस् को निम्नगामी अधः पतन से रोक का ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है—उस शक्ति को गन्दी नाली में बखेरने की अपेक्षा मस्तिष्कीय चेतना में किया जाता है, तो ब्रह्म लोक जगमगाने लगता है यह निरोध का चमत्कार है।
तप साधना का दूसरा पक्ष है—मंथन। समुद्र मंथन की वह पौराणिक आख्यायिका सर्व विदित है जिसमें देव-दानवों ने मिल कर समुद्र मथा था और चौदह बहुमूल्य रत्न पाये थे। जीवन एक समुद्र है। इसमें इतनी रत्न राशी भरी पड़ी हैं जिनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। सिद्धियों और रिद्धियों की गणना अमुक संख्या में की जाती है, पर वह बालकों की अपनी अनुभूति भर है जिसने खोजा उसने उतना पाया बताया। समुद्र बहुत विस्तृत है। बच्चे इसमें कितना घुस सके और कितना पा सके इतने भर से यह अनुमान लगाना उचित नहीं कि समुद्र की समग्र सम्पदा इतनी स्वल्प ही है।
जीवन सिंधु में से श्रेष्ठ रत्नों को निकालने के लिए सामान्य से अधिक पुरुषार्थ एवं साहस की आवश्यकता पड़ती है। इसका जागरण और विकास तप साधना के माध्यम से हो सकता है—होता है। जो इन्हें विकसित कर लेता है वह जीवन की बहुमूल्य संपदाओं का स्वामी बन जाता है—महामानव बन जाता है। प्रखरता का अभाव मनुष्य को सब प्रकार सम्पन्न होते हुए भी दीन हीन ही बनाये रहता है। इस तथ्य के अनेक प्रमाण सामान्य जीवन क्रम में देखे जा सकते हैं। कई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से समर्थ और मानसिक दृष्टि से सुयोग्य होते हैं, पर साहस का अभाव होने से वे कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाते। शंका-कुशंकाओं से ग्रस्त रहने—आपत्तियों की—असफलताओं की संभावना उन्हें पग-पग पर डराती रहती है। थोड़ी-सी कठिनाई अपने पर डरे घबराये दिखाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रगति के उपयुक्त अवसर सामने होने पर भी उन्हें गंवाते और गई-गुजरी स्थिति में आजीवन पड़े रहते हैं। इसके विपरीत साहसी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन एवं उपयुक्त अवसर न होने पर भी दुस्साहस भरे कदम उठाते और आश्चर्यचकित करने वाली असफलताएं प्राप्त करते देखे जाते हैं। ऐसे ही दुस्साहसी व्यक्ति इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम अमर करते देखे जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सफलताएं पाने के लिए ऐसी ही साहसिक मनोभूमि का होना आवश्यक है।
जीवन के हर क्षेत्र में पग-पग पर संघर्ष की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत कठिनाइयों को चीरते हुए ही प्रगति सम्भव होती है। नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। मकान बनाने का कार्य नींव खोदने से आरंभ होता है। खेत को बोने से पहले उसे जोतना पड़ता है। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए जीव जिन पशु-प्रवृत्तियों का अभ्यस्त होता है, उन्हें घटाये-हटाये बिना मानवी गरिमा के अनुरूप गुण-कर्म स्वभाव उपार्जित नहीं किया जा सकता। आन्तरिक अवांछनीयताओं को हटाकर उस स्थान पर उत्कृष्टताओं की स्थापना करने के प्रयोग को साधना कहते हैं। यह साहसिकता के बिना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं। बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए जितना युद्ध कौशल चाहिए उतना ही शौर्य साहस अपने भीतर घुसे हुए काम, क्रोध, लोभ मोह, मद-मत्सर जैसे आत्म शत्रुओं से लड़ने और परास्त करने के लिए आवश्यक होता है। दुर्बल मनःस्थिति के लोग अपनी भीतरी कमजोरियों को जानते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, पर साहस के अभाव में उनके साथ लड़ने का पराक्रम प्रदर्शित नहीं कर सकते। फलतः आत्म-सुधार एवं आत्मनिर्माण का प्रयोजन पूरा कर सकना उनसे बन ही नहीं पड़ता। अपने को असहाय अनुभव करते हैं और थक कर प्रयत्न ही छोड़ बैठते हैं।
बाहरी युद्ध जीतने के भौतिक लाभ हैं किन्तु आंतरिक युद्ध में जीतने से तो विभूतियों का इतना बड़ा भण्डार हाथ लगता है जिसे पाकर मनुष्य जीवन सच्चे अर्थों में सार्थक माना जा सकता है। साधना को संग्राम कहा गया है। ‘साधना समर’ शब्द का अध्यात्म विज्ञान में बार-बार उल्लेख होता है। देवासुर संग्राम के अनेकानेक प्रसंग पौराणिक उपाख्यानों में आते हैं, यह अलंकारिक रूप मनुष्य जीवन के अन्तरंग और बहिरंग क्षेत्रों में सदा होते रहने वाले संघर्षों का ही चित्रण है। दुर्गा सप्तशती और गीता की पृष्ठ भूमि इसी संघर्ष के आधार पर खड़ी है भगवती दुर्गा द्वारा असुरों का संहार और कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से महाभारत का आयोजन प्रकारान्तर से इसी तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि साधना समर के क्षेत्र में प्रवेश किये बिना उन अवरोधों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जो मनुष्य को दयनीय दुर्दशा में डाले रहने के लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी हैं।
भगवान के अवतार के प्रसिद्ध प्रयोजन दी हैं (1) अधर्म का उन्मूलन (2) धर्म का संस्थापन। अनाचार को निरस्त करके ही सदाचार की स्थापना हो सकती है। अस्तु सिक्के के दो भागों की तरह उन्हें परस्पर पूरक एवं अविच्छिन्न भी कह सकते हैं। उद्यान को विकसित करने वाला माली जहां खाद-पानी लगाता है वहां निराई, गुड़ाई, छंटाई, रखवाली जैसी कड़ाई भी बरतता है। आत्मोत्कर्ष के लिए जहां सत्प्रवृत्तियों का विकसित किया जाना, पुण्य प्रयोजनों को अपनाना अभीष्ट है, उतना ही दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए तत्परता बरतना भी आवश्यक है। भगवान के अवतार इस दुहरी क्रिया प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए ही होते रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी प्रगति पथ पर बढ़ने वालों को इसी मार्ग का अवलम्बन करना होता है। संक्षेप में इसे यों कह सकते हैं कि जिसके अन्तःकरण में भगवान की दिव्य ज्योति का अवतरण होगा, उसे अवांछनीयताओं के विरुद्ध लोहा लेने के लिए पराक्रम प्रदर्शित करना होगा और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में जुटना होगा। यह दोनों ही प्रयोजन जिस आन्तरिक साहस द्वारा सम्पन्न होते हैं, उसी को ‘आत्म बल’ कहा गया है। तप साधना का एक उद्देश्य आत्मबल का उपार्जन भी है।
कुविचार मस्तिष्क पर छाये रहते हैं और शरीर को अकर्म करने की आदत पड़ी होती है यदि पुराने अभ्यासों को काटा, उखाड़ा न जाय तो फिर उत्कर्ष के लिए आगे बढ़ चलना कैसे बन पड़ेगा। स्पष्ट है कि कुविचारों को सद्विचारों से ही निरस्त किया जा सकता है। कांटे से कांटा निकालने और विष से विष को मारने की उक्ति प्रसिद्ध है। मस्तिष्क में यदि कामुकता के विचार उठते रहते हैं, तो उनके काटने का एक ही उपाय है कि ब्रह्मचर्य के—पवित्र दृष्टिकोण के समर्थक विचारों को मस्तिष्क में जमा किया जाय। इस मार्ग पर चलने वाले हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, दयानन्द आदि महामानवों के चरित्रों का चिन्तन किया जाय, उस पक्ष के समर्थन वाले तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों को पर्याप्त मात्रा में स्वाध्याय, मनन आदि की सहायता से संग्रह किया जाय। उन पर बार-बार गहराई से विचार किया जाय। कामुकता तथा शालीनता के दोनों पक्षों को अपनी-अपनी बात के समर्थन का अवसर देकर यदि विवेक द्वारा निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह फैसला करने का अवसर दिया जाय तो पुराने अवांछनीय चिन्तन अभ्यास को आसानी से काटा जा सकता है। शारीरिक दुष्प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भी यही बात है। नशा, व्यसन, आलस्य जैसे दुर्गुणों से निपटना, कठोर संकल्प एवं दृढ़ निश्चय से ही सम्भव हो सकता है। व्यक्तित्व का कायाकल्प कर सकने वाले व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शूर-वीर कहे जाते हैं और उन्हीं को भौतिक जगत की प्रत्येक दिशा में बढ़ चलने का द्वार खुला मिलता है।
अण्डा तब फूटता है जब उसके भीतर के बच्चे की अन्तःचेतना उस परिधि को तोड़ कर बाहर निकलने की चेष्टा करती है। प्रसव पीड़ा और प्रजनन की घड़ी तब आती है जब गर्भस्थ शिशु की चेष्टा उस बन्धन को तोड़ कर मुक्ति पाने की आतुर चेष्टा में संलग्न होती है। इन शिशुओं के संकल्प गिरे-परे हों तो वे भीतर ही सड़-गल कर नष्ट हो जायेंगे। प्रगति के लिए पराक्रम और अवांछनीयताओं के विरुद्ध संघर्ष का शौर्य साहस अपना कर ही किसी को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ चलने का अवसर मिलता है। पराक्रम विहीन व्यक्ति को प्रतिपक्षी शक्तियां नष्ट-भ्रष्ट करके रख देती हैं। भगवान बुद्ध ने यों अपने समय के अनाचार से शूर वीरों की तरह लड़ाई लड़ी थी पर पीछे उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का एक सरल पक्ष ही ध्यान में रखा—अहिंसा। यह भुला दिया गया कि आक्रमणकारी हिंसा की दुष्टता से लोहा लिये बिना अहिंसा की रक्षा नहीं हो सकती। हुआ भी यही। अहिंसा की आड़ में कायरता ने अड्डा जमा लिया। लोग जप तप का सरल आश्रय तो पकड़े रहे पर अनीति से जूझने की प्रखरता को व्यर्थ समझने की एकाकी दृष्टि अपनाते रहे। मध्य एशिया के लुटेरों ने इस दुर्बलता को समझा और वे भारत पर चढ़ दौड़े। शौर्य गंवा देने पर वे बहुसंख्यक और साधन-सम्पन्न होते हुए भी थोड़े-से लुटेरों का सामना न कर सके और पराधीनता के पाश में जकड़ गये। हमारी हजार वर्ष की गुलामी आक्रमणकारियों की वरिष्ठता का नहीं—हमारी आन्तरिक दुर्बलता का काला पृष्ठ है—जिसे एकांगी अहिंसा वृत्ति को अपना कर भीरुता एवं कायरता के रूप में स्वभाव गत बना लिया गया था। पराक्रम गंवा बैठा जाय तो मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, चूहे एवं शरीर में घुसे अदृश्य रोग कीटाणु तक अपने अस्तित्व के लिए खतरा बनकर खड़े हो जायेंगे। चोर, उचक्के, गुण्डे, ठग, आततायी अपने ही इर्द-गिर्द भरे पड़े होते हैं और उन्हें जब दुर्बलता का पता चलता है तो अति उत्साहपूर्वक आक्रमण करने के लिए टूट पड़ते हैं। प्रगति के लिए न सही, आत्म-रक्षा तक का उद्देश्य बिना प्रचंड पराक्रम विकसित किये संभव नहीं हो सकता। पराक्रम प्राण का गुण है इसी को पुरुषार्थ भी कहते हैं। प्राणवान पुरुषार्थी को ही पुरुष कहा गया है। नर और पुरुष में अन्तर है। पुरुष शब्द पुरुषार्थी नर और नारी दोनों के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए महापुरुष शब्द के अन्तर्गत महान नारियों की भी गणना होती है। यदि ऐसा न होता तो महान नारियों की उपेक्षा भावना ही समझी जाती अन्यथा महापुरुष की तरह महानारी का भी उल्लेख इतिहास पुराणों एवं शास्त्रों में रहा होता।
आत्म-बल इसी आन्तरिक ऊर्जा का नाम है जो मनुष्य को भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में प्रबल पुरुषार्थ और अनुपम साहस का संचार कर देती है। आत्म-बल हीन मनुष्य कोई भी कड़ा कदम उठाने में झिझकता है। सांसारिक प्रगति हो या आध्यात्मिक प्रगति, दोनों ही स्थितियों में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तपस्वी व्यक्ति में सहज क्रम से ही उसका विकास होता चलता है। कठिनाइयों से भयभीत होने की अपेक्षा तपस्वी उन्हीं में रस लेने लगता है। उस स्थिति में साधक किसी भी सफलता की उचित कीमत चुकाकर उसका अधिकारी बनने की स्थिति में अपने आपको पाता है।
चेतना का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देना योग समझा जाय और क्रिया-कलाप में सुव्यवस्था का आरोपण तप माना जाय। इसके लिए कई तरह के लिये प्रयोगात्मक अभ्यास करने पड़ते हैं। पहलवान बनने के लिये अखाड़े में जाकर छोटी छोटी कसरतों का सिलसिला शुरू करना पड़ता है। कसरतों की खिलवाड़ और दंगल में कुश्ती पछाड़ कर यशस्वी होना दो अलग स्थितियां हैं, पर दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है।
दंगल में कुश्ती पछाड़ना बड़ा ही गौरव की बात समझी जाती है—उसके सामने अखाड़ों में सामान्य कसरत नगण्य लगती है। किन्तु समझदार व्यक्ति जानते हैं कि दंगल की कुश्ती पछाड़ने की स्थिति तक उन्हीं खिलवाड़ जैसे अभ्यासों के माध्यम से पहुंचा जाता है। इस प्रकार जीवन की लौकिक पारलौकिक सफलतायें प्राप्त करने की क्षमता मनुष्य तप साधना द्वारा अर्जित करता है। पौराणिक उपाख्यानों से लेकर वर्तमान काल के महापुरुषों तक के जीवन की अद्भुत सफलताओं के पीछे किसी न किसी तप साधना के आधार की झलक पायी जा सकती है। हम भी उसे जीवन में अपनाकर क्रमशः अधिकाधिक प्रगति के अधिकारी बन सकते हैं।
***