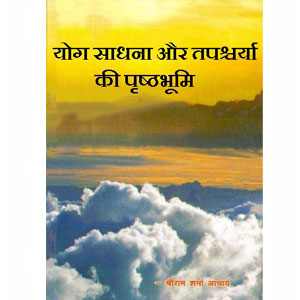योग साधना और तपश्चर्या की पृष्ठभूमि 
योग साधना से चरम लक्ष्य की प्राप्ति
Read Scan Versionयोग का सामान्य अर्थ होता है—जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया अध्यात्म भाषा में ‘योग’ कहलाती है। इसे आरम्भ करने के लिए जिन क्रिया-कलापों को अपनाना पड़ता है उन्हें ‘साधन’ कहते हैं। साधना अपने आप में एक छोटा उपकरण मात्र है। उसका महत्व इसलिए है कि वह ‘साध्य’ को प्राप्त कराने में सहायता करती है। कई लोग साधन को ही ‘साध्य’ समझ बैठते हैं और उन उपचारों को ही योग कहने लगते हैं जो साधना प्रयोजन में प्रयुक्त होते हैं।
आत्मा को परमात्मा से मिला देने के लिए कुसंस्कारों से पीछा छुड़ाना पड़ता है और ईश्वरीय प्रेरणा का अनुगमन करते हुए अपनी अन्तरंग और बहिरंग स्थिति ऐसी बनानी पड़ती है जो ब्राह्मी कहीं जा सके। दूध और पानी एकरस होने से घुल सकते हैं। लोहा और पानी का घुल सकना कठिन है। हम अपने भौतिकतावादी स्तर से ऊंचे उठें और ईश्वरीय चेतना के अनुरूप अपनी क्रिया, विचारणा एवं आस्था को ढालें तो ईश्वर प्राप्ति का जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। वियोग का अन्त योग में होना चाहिए—यही ईश्वर की इच्छा है। बच्चा दिन भर खेलकूद और पढ़ने-लिखने में संलग्न रहे, पर रात को घर लौट आये और एक ही बिस्तर पर सो जाये, ऐसी माता की इच्छा रहती है। परमात्मा भी अपने पुत्र आत्मा से ऐसी ही अपेक्षा करता है। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए—अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें जो चेतनात्मक पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसी का नाम योग साधना है। योग साधना में कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्रिया कृत्य अपनाने पड़ते हैं। इनका उद्देश्य आत्म चेतना को परमात्मा चेतना से जोड़ने वाली मनःस्थिति उत्पन्न करना है। यह तथ्य ध्यान में रखकर चला जाय तो ही लक्ष्य की पूर्ति होना सम्भव है। यदि चेतनात्मक परिष्कार के लिए प्रयत्न न किया जाय और मात्र उन क्रिया-कृत्यों को ही योगाभ्यास मान लिया जाय तो उस भ्रान्ति के कारण घोर परिश्रम करते रहने पर भी कोल्हू के बैल की तरह जहां के तहां बने रहना पड़ेगा।
शारीरिक श्रम में आसन प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा, व्रत, मौन, नेति, धेति, वस्ति, न्यौलि, वज्रोली, कपाल भाति, भूमिशयन, सर्दी-गर्मी सहना, कीर्तन आदि कितने ही उपचार काम में लाये जाते हैं। इनका उद्देश्य स्वस्थता, समर्थता एवं पवित्रता उत्पन्न करना है। ताकि मल भारों से लदे व्यक्ति को आत्मिक प्रगति की लम्बी मंजिल पार करने में सुविधा हो। इसी प्रकार मानसिक उपासनाओं में—जप, ध्यान, नाद, एकाग्रता, तन्मयता, स्वाध्याय, सत्संग आदि साधनों का आश्रय लिया जाता है ताकि चेतना को दिशा एवं प्रेरणा दी जा सके और उसे अपनी जीव ससीमता को ब्रह्म असीमता में घुला देने के लिए आवश्यक प्रकाश एवं प्रशिक्षण मिल सके।
लक्ष्य विहीन साधना मनोरंजक भटकाव ही कहा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाकृत्यों को योगाभ्यास के आधार साधन मानना ही पर्याप्त है। उन कृत्यों को ही जादुई मान बैठना और उनकी प्रवीणता मिल जाने मात्र से लक्ष्य पूरा हो जाना मान लिया जायगा तो यह विशुद्ध भ्रान्ति ही सिद्ध होगी। प्रयत्न यह होना चाहिए कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने पर उपयुक्त भाव चेतना उत्पन्न की जा सके। महत्व तो इस ‘भाव उभार’ का ही है। वह उभरेगा तो गाड़ी आगे चलेगी अन्यथा तथाकथित योगाभ्यासों की हलचलें कुछ समय तक श्रम-साधना में जितनी कुछ जैसी कुछ अनुभूति दे सकती हैं, उसे देकर समाप्त हो जायेंगी। भाव विहीन साधना से शरीर की स्वस्थता और मन की एकाग्रता भले ही कुछ सीमा तक बढ़ सके, आत्मिक प्रगति का लक्ष्य पूरा न हो सकेगा। इसके लिए भावनायें तरंगित करनी पड़ेंगी। भक्ति भावना, शब्द का प्रयोग इसीलिये किया जाता है कि उसमें भावनाओं का तरंगित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके बिना सारे अभ्यास निष्प्राण ही बने रहेंगे। यही कारण है कि क्रियाकृत्यों को सब कुछ मानकर उन्हीं की प्रवीणता के लिए माथापच्ची करते रहने वाले व्यक्ति प्रायः निराश रहते और असफलता की शिकायत करते ही पाये जाते हैं।
योग को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है। चित्त की वृत्तियां ‘प्रेम’ को —वासना, तृष्णा, मोह, अहंता आदि भौतिक लिप्सा लालसाओं की पूर्ति को ही सुखद मानती हैं, उन्हीं की इच्छा करती हैं और उन्हीं में निरत रहती हैं। पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है इस पतनोन्मुख प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए वैसा ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसे कुएं से पानी खींचने अथवा तालाब का पानी टंकी में चढ़ाने के लिए। मन को ढीला छोड़ देने से वह जन्म जन्मान्तरों के संग्रहीत एवं अभ्यस्त पशु प्रवृत्तियों के अस्तबल में अपने आप घुस जायेगा। घड़े से गिरते ही पानी नीचे की ओर बहने लगता है। चित्त का भी, यही स्वभाव है। उसे उलटने का जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसी को ‘चित्त वृत्ति निरोध’ कहा जायगा। महर्षि पातंजलि ने इसी प्रयास को योग कहा है।
कई व्यक्ति चित्त वृत्तियों के निरोध की बात को नहीं समझते और मात्र ‘चित्त निरोध’ को ही योग मान लेते हैं। उनका तात्पर्य ‘एकाग्रता’ से होता है। एकाग्रता होना ही उनकी दृष्टि में योगाभ्यास की सफलता है और उसका न होना असफलता। यह भ्रम है। एकाग्रता एक चीज है और एक धारा दूसरी। एकाग्रता का अपना महत्व और अपना लाभ है—उसका औचित्य और उपयोग समझा जा सकता है, पर एकाग्रता को ही योग का—उपासना का आधार मान बैठना गलत है। एकाग्रता के भी स्तर हैं, मैस्मरेजम, हिप्नोटिज्म में भी एकाग्रता प्रयुक्त होती है और देव प्रतिमा के समक्ष होकर उसकी पूजा, आरती, स्तुति आदि से भी एकाग्रता का पाठ पढ़ा जाता है। पीछे यह बढ़ते-बढ़ते उस स्थिति तक भी पहुंच सकती है जिसे तन्मयता, भाव समाधि, विचार शून्यता आदि का नाम दिया जा सके।
एकाग्रता की स्थिति समय साध्य है, उसके लिए धैर्य और प्रयत्न पूर्वक बहुत समय तक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होगी। वह स्थिति न आये तो भी उतना हर्ज नहीं, जितना समझा जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए मन की दिशा और धारा बदल देने की आवश्यकता है, उतने भर से ‘चित्त वृत्ति निरोध, की—योग की आवश्यकता पूरी होने लगती है।
इसके लिए ‘प्रेय’ की लिप्सा ‘श्रेय’ की आकांक्षा में बदली जानी चाहिए। पेट, प्रजनन भर के लिए जीने में संलग्न पशु स्तरीय प्रवृति को बदल कर आत्मा को परमात्मा स्तर तक विकसित करने की देव स्तरीय प्रवृति में प्रवेश करना चाहिए। आकांक्षाएं बदल जाने से मन की विचारणा और शरीर की कार्य पद्धति में काया कल्प प्रस्तुत हो जायगा। प्रेय की निरर्थकता और श्रेय की सार्थकता में विश्वास बढ़ चले तो उसका प्रभाव कल्पना क्षेत्र तक सीमित न रहकर व्यावहारिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेगा।
जीवन का लक्ष्य समझा जाना चाहिये और प्रगति की दिशा अपनाई जानी चाहिए। निरुद्देश्य जीने से हवा के साथ-साथ उड़ते फिरने वाले पत्तों जैसी दुर्गति होती है। वे यत्र-तत्र सर्वत्र भटकते भर हैं, पहुंचते कहीं नहीं—पाते कुछ नहीं। जीवन का सुनिश्चित लक्ष्य अपूर्णता को पूर्णता में विकसित करना—आत्मा को परमात्मा स्तर तक पहुंचाना ही है। उसे जितनी जल्दी समझा और अपनाया जा सके उतना ही उत्तम है। शरीर रक्षा और परिवार पोषण के लिए उपार्जन तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य भी किये जाने चाहिए किन्तु उतने भर में सीमित न ही बैठा जाय। यह ध्यान पूरी गम्भीरतापूर्वक रखा जाना चाहिए कि सुरदुर्लभ मनुष्य शरीर किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और उसे पूरा करने में ही दूरदर्शी बुद्धिमत्ता है। अन्तःकरण में यह तथ्य निरन्तर जागृत बना रहे तो समझना चाहिए कि उपयुक्त जीवन दिशा मिल गई और उसके प्रकाश में सद्भावनाएं अपनाये रहने तथा सत्प्रवृत्तियों में संलग्न रहने की धारा बह चलेगी। एक दिशा एक लक्ष्य, एक आकांक्षा, एक प्रेरणा यदि निश्चित हो जाय तो फिर शरीर और मन को उसी ओर चल पड़ने की बात बन जाती है और धीरे-धीरे चलते रहने पर भी देर सवेर में मनुष्य वहां जा पहुंचता है जहां पहुंचा देख कर उसका साथी चमत्कार हुआ या देवता का वरदान मिला मानने लगता है।
आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली यही सड़क है। श्रेय की प्राप्ति को लक्ष्य मान कर चलने से चित्त वृत्तियों में पूर्व की अपेक्षा असाधारण परिवर्तन हो जाता है। निकृष्टता उत्कृष्टता की दिशा में उलट पड़ती है इसी ऊर्ध्व गमन को चित्तवृत्ति निरोध कहा जाता है। पतनोन्मुख पशु-प्रवृत्तियां जब उत्थान की दिशा में देव प्रवृत्तियों का रूप बना लेती हैं तो उस स्थिति को योग स्थिति कह सकते हैं।
यहां प्रश्न यह उठता है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने में क्या रुकावट है जिसके लिए योग साधना की आवश्यकता पड़ती है? तत्वदर्शियों ने उसके दो कारण बतलाये हैं। एक है उसका बद्ध होना तथा दूसरा है उसका विकृत होना। लोग के खनिज में लोहा होता है, किन्तु वह लोहे के दूसरे टुकड़े के साथ तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाता। इसी प्रकार रस्सी का सिरा पकड़कर कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। किन्तु यदि वह व्यक्ति उसी रस्सी के सिरे से अपने आपको किसी नीचे की वस्तु से बांध ले तो बन्धन खुले बिना वह चढ़ नहीं सकता। जीव को योग स्थिति में जाने से जो विकृति और बन्धन रोकते हैं उनका स्वरूप समझना तथा उनके निवारण का ढंग भी योग के साधक को समझना चाहिए।
जीवात्मा ईश्वर का अंश है। समुद्र की लहरों और सूर्य की किरणों से उसकी तुलना की गई है। इस भिन्नता को घटाकाश और मठाकाश के रूप में भी समझाया जाता है। घटाकाश अर्थात् घड़े के भीतर की सीमित पोल और मठाकाश अर्थात् विशाल विश्व में फैली हुई पोल। घड़े के भीतर की पोल वस्तुतः ब्रह्माण्ड-व्यापी पोल का ही एक अंश है। घड़े की परिधि से आवृत्त हो जाने के कारण उसकी स्वतन्त्र सत्ता दिखाई पड़ती है, पर तात्विक दृष्टि से वह कुछ है नहीं। घड़े के आवरण ने ही यह पृथक रूप से देखने और सोचने का झंझट खड़ा कर दिया है। शान्त समुद्र में लहरें नहीं उठतीं, पर विक्षुब्धता की स्थिति में वे अलग-सी लगती हैं और उछलती दिखाई पड़ती हैं। सूर्य के तेजस की विस्तृत परिधि ही उसके किरण विस्तार की सीमा है। सूर्य सत्ता का जहां तक जिस स्तर का विस्तार है वहां तक उसी स्तर की धूप का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इस प्रभा विस्तार की जो विभिन्न प्रकार की हलचलें हैं उन्हीं को किरणें कहते हैं। किरणों का सात रंगों में अथवा अल्ट्रावायलेट, अल्फावायलेट एक्स-लैसर आदि में अलग से जाना माना जा सकता है, पर यह विभाजन सूर्य से भिन्न किसी पृथक सत्ता का भान नहीं करता। ऐसे ही उदाहरणों से जीवन और ईश्वर की एकता भिन्नता समझी जा सकती है।
पानी में से असंख्य बुलबुले उठते, तैरते और फिर उसी में समा जाते हैं। विश्व-व्यापी अग्नि तत्व तीली या लकड़ी में प्रकट और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। आग बुझ जाने से वह उसी मूल सत्ता में लय हो जाता है। इन उदाहरणों में भी जीव और ईश्वर की पृथकता एवं एकता का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बड़ा ढेला फूटकर रज-कण के रूप में बिखर जाता है। पानी ऊपर से गिरने पर जमीन से टक्कर खाता है और उसकी बूंदें अलग से छितराती हुई दीखती हैं। जीव और ईश्वर की पृथकता के सम्बन्ध में ऐसे ही उदाहरणों से वस्तुस्थिति समझी जा सकती है। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म ने ‘एकोऽहम् बहुस्याम’ की इच्छा की और उसने अपने आपको टुकड़ों में बखेर दिया। यह बिखराव प्रकृति के साथ संयुक्त हुआ और इसके साथ घुलकर अहन्ता का आवरण अपने ऊपर लपेट बैठा। सूखी मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो वह गीली हो जाती है और उस पर काई तथा दूसरी वनस्पति जमने लगती है। आत्मा के अंश प्रकृति के साथ मिलकर आधे तीतर, आधे बटेर बन जाते हैं। कच्ची धातुएं खदान से मिट्टी मिली स्थिति में निकलती हैं, पीछे उन्हें भट्टी में डालकर शुद्ध किया जाता है। जीव को मिट्टी मिला लोहा कहा जा सकता है। जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय है।
जीव की मूल सत्ता ईश्वरीय है। चेतना का समुद्र इस विश्व में एक ही है। उससे भिन्न या प्रतिपक्षी दूसरी कोई सत्ता देवी-देवताओं के या जीवों के रूप में कहीं नहीं है। तत्ववेत्ताओं ने जाना है—‘यहां केवल एक है दूसरा नहीं।’ जीव की पृथकता प्रकृति के समन्वय से है। प्रकृति के तीन स्तर सत, रज, तम कहलाते हैं, इन्हीं तीनों की तीन परतें जीव के ऊपर चढ़ जाती हैं और वे तीन शरीर कहलाती हैं। स्थूल शरीर अर्थात् हाड़-मांस की जन्मने मरने वाली काया। सूक्ष्म शरीर अर्थात् बुद्धि संस्थान, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय, अपने बिराने का अन्तर करने वाला मस्तिष्कीय विचार विस्तार। कारण शरीर अर्थात् मान्यताओं एवं भावनाओं का समुच्चय—अन्तरात्मा। जिसे अन्तःकरण भी कहा गया है। इन तीर शरीरों की यों प्याज के छिलके, केले के तने या एक के ऊपर एक पहने हुए वस्त्रों से तुलना की जाती है, पर यह उपमा बहुत ही अधूरी है। कारण कि यह सब आवरण एक दूसरे से प्रथक हैं जबकि शरीर एक-दूसरे के साथ इस प्रकार घुले हुए हैं जैसे दूध में घी, सरसों में तेल। प्रयत्न पूर्वक इन्हें पृथक किया जा सकता है। मृत्यु के उपरान्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध टूट जाता है। क्लोरोफार्म सुंघा देने या गहरी नींद आ जाने पर सूक्ष्म शरीर का चेतन भाग मूर्च्छित हो जाता है, अचेतन भर जागता रहता है। समाधि अवस्था में सूक्ष्म शरीर को कारण से अलग किया जा सकता है। मुक्ति अवस्था में कारण शरीर का आवरण भी छूट जाता है और बूंद समुद्र में समा जाने की तरह आत्मा का लय परमात्मा में हो जाता है। इस प्रकार यह तीनों ही आवरण हटाये तथा मिटाये जा सकते हैं, पर सामान्य स्थिति में वे परस्पर घुले-मिले ही रहते हैं।
जीव को इन आवरणों में लिपटे रहने से कई तरह के—कई स्तर के सुख मिलते हैं, इसलिए वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता फलतः ‘वद्ध’ अवस्था में बना रहता है। स्थूल शरीर में कई प्रकार के वासनात्मक सुख हैं। सूक्ष्म शरीर में कल्पना लोक के मनोरम स्वप्न, विनोद, मनोरंजन, सफलता, पद, सम्मान, वैभव आदि के बुद्धि-विलास के अनेकों साधन मौजूद हैं। कारण शरीर में ‘अहंता’ की गहरी परतें जमी हैं। ‘मैं’ अत्यन्त प्रिय है। इस ‘मैं’ की परिधि में जितना क्षेत्र आता है, वह मेरा बन जाता है और जिस प्राणी या पदार्थ पर यह ‘मेरापन’ आलोकित होता है वह भी प्रिय लगने लगता है। आकांक्षाओं की उमंग इसी केन्द्र से उठती है। मान्यताओं की आस्था और संवेदनाओं की पुलकन खट्टी-मीठी गुदगुदी तो है, पर कुल मिलाकर वह है—मधुर। जीवन में प्रिय-अप्रिय प्रसंग आते-जाते रहते हैं, पर कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है जिसके कारण इन तीनों शरीर आवरणों को छोड़ने को मन नहीं करता। फलतः जीव सत्ता का ऐसा सघन अस्तित्व बन जाता है जिसे स्वतन्त्र भी कहा जा सकता है।
दर्शन-शास्त्र के सभी पक्षों ने ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का अस्तित्व तो माना है, पर उनके पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में अपने अपने विचार भिन्न रूप से व्यक्त किये हैं। त्रैत, द्वैत, और अद्वैत मान्यताओं में इसी प्रकार का मतभेद है। त्रैतवादी कहते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति की तीनों सत्ताएं अनादि एवं स्वतन्त्र हैं—उनका सह अस्तित्व भर है। द्वैतवादी, ब्रह्म और माया-पुरुष और प्रकृति की दो सत्ताएं मानते हैं, उनकी दृष्टि में जीव का इन दोनों का समन्वय ऐसा ही है जैसा दिन और रात के मिलन से उत्पन्न हुआ संध्या काल। अद्वैत मत में एक ही ब्रह्म चेतना की सत्ता को जड़ और चेतन के रूप में माना गया है। प्रकृति ब्रह्म का विकार है और और यहां जो कुछ दीख भास रहा है वह बुद्धि विपर्यय का ऐसा ही जादू है जैसा इन्द्र धनुष का अथवा स्वप्न संसार का दीखना। इस स्थिति को भ्रांति अथवा माया कहा गया है।
इन्हें नाम कुछ भी दिया जाय और इनकी दार्शनिक व्याख्यायें चाहे जितने ढंग से की जायें किन्तु यह तथ्य अपरिवर्तित ही रहता है इस मनुष्य को विवशता से ऊपर उठने तथा चरम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना ही चाहिए। योग का साधक यही करता है। योगी अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर तीनों ही को ही अवांछनीयताओं से ‘मुक्त’ करके वांछनीयता से ‘युक्त’ करने का प्रयास करता है। उसके लिए तीनों शरीरों के पूर्ण संस्कारों को साधना अभ्यास द्वारा छुड़ाकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर सही दिशा में नियोजित करता है। इस दृष्टि से योग साधना में एक पक्षीय क्रिया काण्डों तक सीमित न रहकर क्रिया विचारणा और भावना का समुचित समावेश रहता है।
हमें योग स्थिति से वंचित रखने वाली हमारी पराधीनता—मात्र चिर-संचित संस्कारों की है जो स्वभाव बनकर हमारे चिन्तन एवं कर्म को अपने ढर्रे पर चलाती है—अपनी लाठी से हांकती है। शरीर को यह पराधीनता, वासना के बन्धन में बांधकर बेतरह घसीटती है उसका स्वास्थ्य चौपट करती है, दीर्घजीवन से वंचित करती है और सत्कर्म निरत रहकर समृद्धियां, सफलताएं प्राप्त करने के स्थान पर ऐसा कुछ करते रहने में लगाती है जिनके कारण रुग्णता, निन्दा, असफलता, दरिद्रता, कुरूपता जैसी विपन्नताएं ही आये दिन सामने खड़ी रहती हैं। विवेक कई बार सोचता है कि अपनी गतिविधियों में अमुक प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। किन्तु औचित्य समझते हुए भी वैसा कुछ बन नहीं पड़ता। आदतें इतनी जबरदस्त सिद्ध होती हैं कि उपयोगी सुधार के मनसूबे एक कोने में रखे रह जाते हैं और आदतें अपनी बेढंगी राह पर शरीर को घसीटती चली जाती हैं और वे काम कराती हैं जिनके लिए पीछे पश्चाताप ही करना शेष रह जाता है। यदि आदतें शरीर का संचालन न करें, विवेक के हाथ से नियन्त्रण, संचालन किया जाने लगे तो स्वास्थ्य, सौन्दर्य, दीर्घजीवन जैसी उपलब्धियां तो अति साधारण हैं, समर्थ काया से अभीष्ट प्रयोजनों में आश्चर्यजनक सफलताएं देने वाले पराक्रम पुरुषार्थ का अभिनव स्रोत खुल सकता है और उसके फलस्वरूप जो जीवन लाभ मिल सकता है, उसकी कल्पना मात्र से आंखें चमकने लगती हैं। दुर्बल शरीर इन्द्रिय सुख की लिप्सा भर में लगा रहता है, साधन उपस्थित होने पर भी वह उनका समुचित आनन्द नहीं ले सकता। भोजन का आनंद कड़ाके की भूख लगने वाले को ही मिल सकता है। रतिक्रीड़ा एवं गहरी निद्रा का लाभ शरीर पर नियंत्रण रख सकने वाले ही भोगते हैं। आलस्य, प्रमाद को भगाकर व्यवस्थित दिनचर्या बनाना और उस पर निष्ठापूर्वक आरूढ़ रहना—सफलताओं का प्रधान आधार माना गया है। शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, भौतिक जगत से सीधा सम्बन्ध उसी का है। समर्थ शरीर ही भौतिक उपलब्धियों का केन्द्र होता है।
अपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग भौतिक की तरह आत्मिक प्रगति में भी आवश्यक है। इसी लिए योग साधना में शरीर को स्वस्थ तथा आत्म नियंत्रित बनाने के लिए अनेक साधनाओं का उल्लेख मिलता है।शरीर क्षेत्र की साधनायें चाहे हठयोग सम्मत हों चाहे कर्मयोग सम्मत उनका उद्देश्य शरीर को आत्म नियंत्रित बनाकर सही उद्देश्य की ओर नियोजित करने की स्थिति तक पहुंचाना ही है। शरीर मत चमत्कारों की दृष्टि से उन्हें अपने लक्ष्य से भटक जाना ही कहा जाता है। यह तो एक पक्ष हुआ योगी को तो अन्य पक्षों पर भी समान रूप से ध्यान देना होता है।
सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र में हमारा चिन्तन उस ढर्रे में ढला हुआ होता है, जिसकी प्रतिक्रिया ही हमें अर्धविक्षिप्त स्तर का बनाये रहती है। कितने प्रकार की सनकें, कितने वहम, कितने भ्रम मस्तिष्क में लदे होते हैं यदि उन्हें ठीक तरह समझा जाय तो प्रतीत होगा कि विवेकवान व्यक्ति की तुलना में ‘चालू आदमी’ निस्सन्देह अधपगला होता है। लोक-प्रवाह का संशोधन करने अवतारी आत्माएं उतरती हैं उनके चले जाने के बाद फिर विकृतियां भरने लगती हैं और सामाजिक प्रचलनों में गन्दे नाले जैसी गन्दगी भरती चली जाती हैं। जन मान्यताएं—लोगों के प्रचलित ढर्रे ही अपने को सुहावने लगते हैं। कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं, अन्धविश्वासों के सहारे न जाने कितनी उपहासास्पद भ्रांतियां मस्तिष्क में जड़ जमाकर बैठ जाती हैं। लोगों में प्रचलित भ्रष्टाचार अपने को भी ललचा लेता है। विकृत चिन्तन के कारण मनुष्य न सोचने योग्य सोचता है और बाल बुद्धि की योजनाएं बनाकर उनमें बहुमूल्य विचार शक्ति को नष्ट करता रहता है। चिंता, निराशा, खीज, आवेश, उत्तेजना, निष्ठुरता, घबराहट, कायरता, कृपणता, ईर्ष्या, द्वेष, आत्म–हीनता, उद्दण्डता जैसे अनेकों मानसिक रोग मस्तिष्क को घेरे रहते हैं और सौ रोगों से ग्रसित शरीर की जो दुर्गति होती है वैसा ही वे मनोविकार, विचार संस्थान को, सूक्ष्म शरीर को बनाये रहते हैं। यह मनोगत कुसंस्कारों की चिन्तन विकृतियों की, पराधीनता है जिसके कारण हर दृष्टि से ‘अद्भुत’ से ‘अद्भुत’ विचारणा सर्वनाश के गर्त में गिरती और नष्ट होती रहती है।
यदि कुसंस्कारों के बन्धनों से मस्तिष्क को छुटकारा मिल सके तो प्रस्तुत चिन्तन तन्त्र का सुव्यवस्थित सदुपयोग करके कोई भी व्यक्ति विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, दूरदर्शी, मनीषी बन सकता है। विचारणा को सन्मार्गगामी बना सकने वाले व्यक्ति—सामान्य साधनों के बल पर—सामान्य परिस्थितियों में रहते हुए—व्यक्तित्व को परिष्कृत ढांचे में ढाल सकते हैं और महामानवों की श्रेणी में गिने जा सकने की स्थिति में सरलतापूर्वक जा पहुंचते हैं। ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन तत्व का विश्लेषण करने पर विशेषता एक ही दिखाई पड़ती है कि उन्होंने अपने चिन्तन तन्त्र को व्यवस्थित किया, अभ्यस्त विचार पद्धति का नये सिरे से पर्यवेक्षण किया, अनौचित्य को साहसपूर्वक सुधारा और विवेक का आश्रय लेकर विचारणा को उच्चस्तरीय बनाया। लोक-प्रवाह के विपरीत आदर्शवादी मौलिकता अपनाई, फलस्वरूप उनका चिन्तनात्मक काया-कल्प हो गया। आरम्भ में ऐसे लोगों का मखौल बनता और विरोध होता है, पर जब वे अपनी निष्ठा का परिचय देते हैं तब दुनिया उनके चरणों में झुक जाती है और सिर आंखों पर बिठाकर भाव भरी श्रद्धांजलि समर्पित करती है।
परिष्कृत सूक्ष्म शरीर—चिन्तन की उत्कृष्टता के कारण स्वयं हर घड़ी सदा सन्तुष्ट, उल्लसित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। अवांछनीय मानसिक भार से छुटकारा पाने के कारण उसकी सूझ-बूझ, दूरदर्शी, तत्वदर्शी बन जाती है और उसका लाभ न केवल सम्पर्क क्षेत्र को वरन् समस्त संसार को मिलता है।
मस्तिष्क का कुल मिलाकर प्रायः सात प्रतिशत भाग काम में आता है, शेष 93 प्रतिशत प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। उसे जागृत करना अपने भीतर की असंख्यों अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास कर लेना है। मस्तिष्क की तुलना का चमत्कारी सूक्ष्म यन्त्र इस संसार में और कोई नहीं है, इसे यदि प्रयत्नपूर्वक सक्षम बना लिया जाय तो कालिदास जैसे मन्द बुद्धि भी मूर्धन्य विद्वान बन सकते हैं। चमत्कारी सिद्धियों के नाम से कितने ही विशिष्ट कौशल कई सिद्ध पुरुषों में यदा कदा देखे जाते हैं यह और कुछ नहीं जादू की पिटारी—मस्तिष्कीय चेतना की फुलझड़ियां मात्र हैं। इन्द्रिय शक्ति से—मनःशक्ति से हम परिचित हैं, इसलिए उसके द्वारा दैनिक जीवन में प्रस्तुत होते रहने वाले चमत्कारों को ‘सामान्य’ माना जाता है। अचेतन अविज्ञात है इसलिए उसकी जागृति अतीन्द्रिय शक्ति अद्भुत—अलौकिक लगती हैं, पर वस्तुतः चमत्कार जैसी कोई चीज इस संसार में है नहीं। जो कुछ है प्रकृति व्यवस्था के पूर्णतया अनुकूल ही है। चमत्कारी सिद्धियां भी प्रसुप्त अतीन्द्रिय क्षमता का ऐसा जागरण है जो आमतौर से देखा, सुना नहीं जाता। ऐसे तो नये आविष्कार भी कुछ दिन तक चमत्कार ही कहे जाते रहे हैं।
तीसरा आधार—कारण शरीर की चेतना की आस्थाएं सुधर जाने से मनुष्य महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा बन सकता है। यह वह ध्रुव केन्द्र है जहां आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक पतला सा सम्बन्ध सूत्र जुड़ा हुआ है उसे तनिक सा और परिष्कृत कर दिया जाय तो ब्रह्म चेतना का—जीव चेतना विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर सकता है और ऐसे आदान-प्रदान का पथ-प्रशस्त कर सकता है जिसके आधार पर नर में नारायण का अवतरण प्रत्यक्ष देखा जा सके। ऐसी स्थिति में पहुंची हुई आत्माओं की देव संज्ञा होती है। देवताओं की अलौकिकता कथा पुराणों में भरी पड़ी है। उन्हें इन देव पुरुषों में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।
इस स्तर को लाने के लिए योग साधक को चिन्तन तथा भावना परक साधनायें करनी पड़ती हैं। मनुष्य की विचार क्षमता और भाव क्षमता स्थूल क्षमता की अपेक्षा कई गुनी अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी दिशा अधोगामी आकर्षणों से हटाकर उच्चस्तरीय उद्देश्यों के साथ जोड़ना योगी को कुशलता और साधना की प्रखरता पर निर्भर करती है। इसके लिए अनेक चिन्तन तथा अनुभूति परक ध्यान साधनायें की जाती हैं। उनके सहारे जीव अपने को संसारी न समझकर ईश्वर का अंश प्रतिनिधि मानने-समझने लगता है। यह एकता की अनुभूति—उसका चिन्तन योग साधना का महत्वपूर्ण अंग है।
सीमा संकीर्णता को अवास्तविक मानने से व्यक्तिवाद पर अवलम्बित स्वार्थपरता घटती चली जाती है। अपने को बड़ी मशीन का एक छोटा पुर्जा भर समझने से यह बात ध्यान में रहती है कि उसकी निजी उपयोगिता भी पूरी मशीन का अंग बनकर रहने में ही है। अलग निकलकर अलग से—अलग बड़प्पन और सुखोपभोग की बात सोची जायगी तो यह पृथकता अपनाकर कुछ लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। हानि ही होगी। घड़ी से अलग निकल कर एक पुर्जा बाजार में बिकने चला जाय तो उसे कोई दो कौड़ी का न पूछेगा और मिलने पर उपेक्षापूर्वक इधर-उधर पटक देगा, पर यदि वह पूरी घड़ी के साथ हो तो घड़ी को मिलने वाले सम्मान में वह भी समान रूप से भागीदार बना रहेगा। पृथकतावादी स्वार्थपरता पर अंकुश लगाने और समूहवादी गतिविधियां अपनाने में यह एकता का दर्शन बहुत काम करता है।
अपनापन ही प्यारा लगता है। यह आत्मीयता जिस पदार्थ अथवा प्राणी के साथ जुड़ जाती है, वही आत्मीय परमप्रिय लगने लगता है। अपनेपन का दायरा छोटा हो तो मात्र शरीर की—बहुत हुआ तो परिवार की सुख सुविधा सोची जाती रहेगी। वह थोड़ा-सा क्षेत्र ही अपना प्रतीत होगा और उतने तक ही प्रिय लगने की परिधि सीमित बनकर रह जायगी। यह क्षेत्र जितना अधिक बढ़ेगा, उतनी ही प्रियता की परिधि विस्तृत होती चली जायगी। सभी अपने लगेंगे तो अपना परिवार अत्यन्त सुविस्तृत बन जायगा। प्रिय पात्रों की मात्रा जितनी ही बढ़ती है उतना ही सुख सन्तोष मिलता है यदि व्यापक क्षेत्र में आत्मीयता विस्तृत करली जाय तो अपनेपन का प्रकाश बढ़ता जायगा और उस सारे क्षेत्र का वैभव परमप्रिय लगने लगेगा। उन्नति में—वृद्धि और विस्तार में हर किसी को गर्व गौरव अनुभव होता है। बड़े उत्तरदायित्व समझना ही बड़प्पन का चिन्ह है, यह अनुभूतियां उन्हें सहज ही मिल सकती हैं जो सीमा बन्धनों की तुच्छता को निरस्त करके समष्टि के साथ जुड़े हुए कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए कटिबद्ध होता है।
एकता का दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि अंशी के सारे गुण सूक्ष्म रूप से अंश में विद्यमान रहते हैं। अस्तु, परमात्मा की समस्त विशेषताएं तथा सम्भावनाएं आत्मा में विद्यमान हैं और उन्हें विकसित करने के साधन जुटाकर उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। चिनगारी में वे सभी सम्भावनाएं मौजूद रहती हैं जो दावानल में पाई जाती हैं। विशाल वृक्ष का सारा ढांचा बीज के भीतर मौजूद है। प्राणी की आकृति और प्रकृति का अधिकांश स्वरूप उस नन्हे से शुक्राणु में पूरी तरह मौजूद रहता है जो आंखों से दिखाई तक नहीं पड़ता। ब्रह्माण्ड के ग्रह-नक्षत्र जिस नीति-रीति पर अपना क्रियाकलाप चला रहे हैं उसी का अनुकरण सौर-मण्डल करता है और उसी लकीर पर अणु-परमाणुओं के परिभ्रमण प्रयास चलते हैं। छोटे से परमाणु के भीतर एक पूरे सौरमण्डल का नक्शा देखा जा सकता है। एटम के भीतर काम कर रहे—इलेक्ट्रोन, प्रोट्रॉन, न्यूट्रोन आदि की भ्रमण गतियां तथा कक्षाएं लगभग वैसी ही है जैसी कि सौर-मण्डल के ग्रह-उपग्रहों की।
इस तथ्य को समझ लेने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव की मूलसत्ता—गुणों की दृष्टि से ईश्वर के समतुल्य ही है। इस सम्भावना को विकसित करना मनुष्य जीवन में ही सम्भव हो सकता है। अस्तु उच्च पद प्रदान करने में नियोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की तरह ही अपना मनुष्य जीवन मिला हुआ है। परीक्षा में भाग लेने का अवसर जिन्हें मिला है वे अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ परायणता का परिचय देकर उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करते और प्रतियोगिता जीत कर उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसा ही अवसर मनुष्य जीवन के रूप में भी मिला हुआ है। उसकी सार्थकता इसमें है कि अपने छोटे-से जीवात्मा स्तर को विकसित करके महात्मा देवात्मा की कक्षायें पार करते हुए परम आत्मा उत्कृष्टतम आत्मा बनने की पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करे। उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श कर्तृत्व की उदात्त रीति नीति अपनाने वाले ही इस महान् जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते देखे जाते हैं।
मनुष्य जीवन भगवान का प्राणी को दिया गया सबसे बहुमूल्य उपहार है। इससे अधिक महत्वपूर्ण चेतन संरचना उसके भण्डार में और कोई नहीं है। इसे अनुपम और अद्भुत कह सकते हैं। बोलना, सोचना, शिक्षा, कला, आजीविका—उपर्जान, भोजन निश्चिन्तता, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, वाहन, परिवार, समाज, शासन, कृषि, पशुपालन, वैज्ञानिक उपकरण एवं अनेकानेक सुख-साधनों की सुविधा सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है। यहां यह प्रश्न उठता है कि सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं। एक समदर्शी पिता को अपनी सन्तानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और समान अनुदान देने चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मनुष्य को ही इतना अधिक दिया गया और अन्य प्राणी उससे वंचित रखे गये? यदि यह सब विभूतियां मात्र मौज मजा करने के लिए ही मनुष्य को मिली होतीं तो निश्चय ही इसे अन्याय और पक्षपात कहा जाता, किन्तु परमात्मा न तो ऐसा है और न ऐसी नीति अपना सकता है जो उसके महान गौरव पर उंगली उठाने का अवसर देती हो। मनुष्य को अधिक विश्वस्त—अधिक प्रामाणिक और अधिक समझदार बड़ा पुत्र माना गया है और उसके हाथ में वे अतिरिक्त साधन सौंपे गये हैं, जिनके सहारे वह ईश्वर के इस सुरभ्य उद्यान संसार को अधिक सुन्दर, अधिक सुविकसित, अधिक समुन्नत और अधिक सुसंस्कृत बना सके।
खजांची के पास ढेरों सरकारी रुपया रहता है, शस्त्र भाण्डागार का स्टोरकीपर सेना के हथियार और गोला-बारूद अपने ताले में रखता है, मिनिस्टरों को अनेकों सुविधा साधन एवं अधिकार मिले होते हैं। यह सब विशुद्ध रूप से अमानतें हैं। इन्हें निजी लाभ के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। खजांची, स्टोरकीपर, मिनिस्टर आदि यदि अपने अधिकार की वस्तुओं को निजी उपयोग में खर्च करने लगें तो यह उनका अपराध माना जायगा और दण्ड मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को जो मिला है वह संसार को अधिक सुखी समुन्नत बनाने के लिए मिली हुई धरोहर के रूप में है। उसमें से औसत नागरिक के स्तर का निर्वाह भर अपने उपयोग में लिया जा सकता है इसके अतिरिक्त समय, श्रम, ज्ञान एवं धन के, पद प्रभाव आदि के रूप में वैभव मिला है, उसका जितना अंश शेष रह जाता है उसे लोक-मंगल के लिए नियोजित किये रहना मनुष्य जीवन का दूसरा प्रयोजन है।
पूर्णता प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हुए अनुकरणीय, आदर्श एवं पवित्रतम देव जीवन जिया जाय और शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक उपलब्धियों में से न्यूनतम अंश अपने लिए लेकर शेष का परमार्थ प्रयोजनों में उपयोग किया जाय यही है ईश्वर प्रदत्त सुर-दुर्लभ मानव जीवन के अलभ्य अवसर का श्रेष्ठतम उपयोग। राजघरानों में यह प्रथा थी कि बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाया जाता था और वह युवराज ही समयानुसार पिता के सारे उत्तरदायित्वों को वहन करता था छोटे भाई-बहनों की सुव्यवस्था का भार भी उसी के कन्धे पर रहता था। समझा जाना चाहिए कि राजाधिराज परमेश्वर का जेष्ठ पुत्र—युवराज—मनुष्य है उसे अन्य जीव-धारियों की तुलना में जितना कुछ अधिक मिला है वह सब विशेष उद्देश्य के लिए हैं। उसे विलासिता, संग्रह अहंकार के उद्धत प्रदर्शन एवं औलाद के लिए मुफ्त का धन छोड़ जाने जैसे हेय प्रयोजनों में खर्च नहीं किया जाना चाहिये। जमानत को धरोहर को उसी प्रयोजन में लगाया जाना चाहिये जिसके लिए वह मिली है।
शरीर और मन जीवन रूपी रथ के दो पहिए—दो घोड़े हैं। इन्हें काम करने के दो हाथ—आगे बढ़ने के दो पैरों से उपमा दी जा सकती है। अन्तःकरण की आस्था एवं आकांक्षा के अनुरूप यह दोनों ही स्वामिभक्त सेवक सदा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। शरीर की अपनी स्वतन्त्र कोई सत्ता या इच्छा नहीं। वह जड़ है। इन्द्रियां भी जड़ पंचतत्वों से बनी है। अन्तःकरण में जैसी उमंगें उठती हैं, उसी दिशा में शरीर की क्रियाशीलता चल पड़ती है। इसी प्रकार मन भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसमें सोचने का गुण तो है, पर क्या सोचना चाहिये? यह निर्धारण करना अन्तःकरण का काम है। सज्जनों का चिन्तन एवं कर्तृत्व एक तरह का होता है और दुर्जनों का दूसरी तरह का। इसमें दोनों के शरीर और मन सर्वथा निर्दोष होते हैं। अन्तः प्रेरणा का निर्देश बजाते रहना भर उनका काम है। इसलिये शरीर को दुष्कर्म करने या मन को दुर्बुद्धिग्रस्त होने का जो दोष दिया जाता है वह अवास्तविक है। इन दोनों वाहनों को प्रेरणा एवं दिशा देने का काम अन्तःकरण रूपी सारथी का है।
शरीर में क्रिया, मन में विचारणा और अन्तरात्मा में भावना काम करती है। भावनाओं को ही श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, मान्यता आदि के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सबके समन्वय से आकांक्षा उभरती है और फिर उसी की निर्देशित दिशा में शरीर और मन के सेवक काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं।
आत्म-ज्ञान का अर्थ है अन्तरात्मा के गहन स्तर में यह अनुभूति एवं आस्था उत्पन्न करता रहे कि हम सत्, चित्त, आनन्द परमात्म सत्ता के अविच्छिन्न अंग हैं हमें पूर्णता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम जीवन क्रम अपनाना है और जो उपलब्ध है उसे लोकहित के लिए प्रयुक्त करना है। आत्म-ज्ञान की भूमिका में जगा हुआ जीवात्मा संकीर्ण स्वार्थ परता की परिधि को लांघकर सब में अपने को और अपने में सबको देखता है, इसलिए उसके सामने व्यक्तिवादी, आपाधापी फटकने भी नहीं पाती, जो सोचता और करता है उसमें व्यापक लोकहित की—सदुद्देश्यों को कार्यान्वित करने की—भावना काम करती है। कहना न होगा कि आत्मबोध ले लाभान्वित आत्माओं को प्रत्येक विचारणा और प्रत्येक क्रिया-पद्धति में मात्र आदर्शवादिता ही उभरती; छलकती दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग अभावग्रस्त और संकटग्रस्त हो सकते हैं, पर अन्तःकरण में उन्हें असीम आनन्द और सन्तोष की अनुभूति हर घड़ी होती रहती है।
भगवान बुद्ध को जिस दिन आत्म-ज्ञान हुआ, उसी दिन से दिव्य मानव बन गये। जिस वट-वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मबोध हुआ था उसकी टहनियां काट-काटकर उनके अनुयायी अपने-अपने क्षेत्रों में ले गये और वहां उसकी मूर्तिमान देवता के रूप में स्थापना की। इसका तात्पर्य है बुद्ध को सामान्य राजकुमार से भगवान बना देने का श्रेय उस आन्तरिक जागरण को ही दिया गया, जिसे आत्मबोध के रूप में पुकारते हैं। यह उपलब्धि जिसे भी मिल सकेगी वह उसी मार्ग पर चलने वाला और वैसा ही सत्परिणाम प्राप्त करने का अधिकारी माना जायेगा।
योग साधना में केवल चिन्तन तक ही सीमित नहीं रहा जा सकता। भाव संस्थान में उभार आये बिना योग अधूरा ही रह जाता है। भाव प्रखरता जितनी तीव्र होगी योग की सफलता भी उतने ही अंशों में बढ़ती चली जायेगी। जो साधनायें सहज क्रम में कठिन और श्रम साध्य लगती हैं वही भाव जागरण होते ही आनन्ददायक और स्वाभाविक हो जाती हैं। उसमें अपने प्रियतम प्रभु से मिलन का रस मिल जाता है। मनुष्यों में भी दो प्रेमीजन जब मिलते हैं तो भाव-विभोर हो जाते हैं और आनन्दातिरेक का अनुभव करते हैं। भाव भरी पुलकन केवल विश्वस्त, परमप्रिय एवं आत्मीयों के मिलन पर ही उभरती है। इसलिए भगवान के प्रति अत्यन्त उच्चस्तरीय मान्यतायें एवं भावनायें रखकर पुलकन भरे मिलन का—एक दूसरे में आत्मसात् हो जाने की गहन आस्था की अनुभूति को भक्तियोग कहते हैं। लययोग इसी को कहा गया है। आत्म-समर्पण तादात्म्य भी इसी का नाम है। जीवन मुक्ति का वर्णन करते हुए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य के चार भेदों में इसी स्थिति का विवेचन किया गया है। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की अनुभूति, नदी का समुद्र में विलय, अग्नि में आहुति द्रव्य, दीपक पर पतंगों का जलना जैसे उदाहरण देकर इसी भाव स्तर का स्वरूप समझाया जाता है। गोपियों का कृष्ण की बंशी ध्वनि पर थिरकने वाले रास नृत्य में इन्द्रिय समूह एवं चिन्तन धाराओं का परब्रह्म के उदात्त संकेतों का अनुगमन ही है। ‘मैं’ और ‘तू’ में से एक को मिटा देने की बात सूफी सन्त और भक्तयोगी एक स्वर से कहते रहे हैं। मैं मिटता है तो तू रह जाता है। ‘‘मेरा मुझ को कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर’ की—’’अपनी खुदी मिटा दे तेरा खुदा मिलेगा की—अनुभूति भक्तियोग में होती है। इसी तथ्य को थोड़े से शब्दों को उलट-पुलट में दूसरी तरह भी कहा जा सकता है—अयमात्माब्रह्म-प्रज्ञानं ब्रह्म तत्वमसि सच्चिदानन्दोहम्—‘शिवोहम् की मान्यता में ‘तू’ मिट जाता है और मैं रह जाता है दोनों ही स्थितियों में एकता, एकरूपता—एक सत्ता का प्रतिपादन है। भक्त और भगवान के एक बन जाने की बात है। अयमात्मा ब्रह्म का आत्मा-निकृष्ट नर-पशु नहीं होता वरन् उसकी क्रिया विचारणा एवं आकांक्षा ठीक वैसी ही होती है, जैसी परमेश्वर की। इससे नीची स्थिति में ‘शिवोहम्’ की बात कहां बनती है। परमात्मा स्तर पर पहुंचा हुआ आत्मा अपनी अहंता को पूरी तरह खो चुका होता है। उसके साथ जुड़े हुए संकीर्ण स्वार्थपरता के सारे बन्धन भी समाप्त हो जाते हैं ऐसा मनुष्य लोभ, मोह के बन्धनों से विरक्त होकर वैरागी जीवन जीता है और उच्चस्तरीय प्रेरणाओं को ईश्वर के संकेत मानकर उनका अनुगमन करता है।
इसके लिए मात्र मस्तिष्क द्वारा सम्भव होने वाले ध्यान चिन्तन से काम नहीं चलता वरन् प्रियतम के साथ एकाकार होने के भावोन्माद को जगाना पड़ता है। मीरा, चैतन्य, रामकृष्ण, परमहंस आदि में यह उन्माद मुखरित हो उठा था। ऋषियों में तत्वदर्शी मनीषियों में यह सौम्य शांत रस बनकर रचनात्मक प्रयोजनों में लगा रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वह बुद्ध और गांधी की तरह सामयिक समस्याओं के समाधान में अवतारी महामानवों की भूमिका भी सम्पन्न करता है।
इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति का भावोन्माद उभारने वाले साधक भी देखे गये हैं दूसरे अत्यन्त शान्ति पूर्वक हिमालय में अपनी काया को गला कर हिम रूप बना देने जैसी अनुभूतियों से भी काम चला लेते हैं। तात्पर्य द्वैत को मिटा देने से है। आत्मा और परमात्मा की एकता की भावना जिस भी भाव-प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न की जाय, वे सभी भक्तियोग के—लययोग के अन्तर्गत गिनी जायेगी।
***