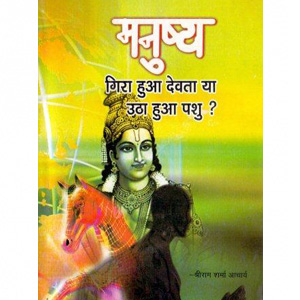मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु ? 
गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु?
Read Scan Version
मनुष्य का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है, धर्म उसे गिरा हुआ देवता कहता है और विज्ञान उसे ‘उठा हुआ पशु’ बताता है। देखना यह है कि दोनों प्रतिपादनों में यथार्थता किसके साथ है।
आदम और हव्वा स्वर्ग में रहते थे उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अभक्ष्य खाया और जमीन पर आ गिरे। उनके वंशज मनुष्य कहलाए। देवता और अवतारों का धरती पर उतर का मनुष्य शरीर धारण करना और सन्तानोत्पादन में संलग्न होना। प्रायः इसी से मिलती जुलती कथा गाथाएं समस्त धर्मों में प्रचलित हैं, जिनमें आदि मानव के अस्तित्व का आरम्भ किस प्रकार हुआ, इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है। यह मान्यताएं बताती हैं कि मनुष्य गिरा हुआ देवता है। स्वर्ग लोक के देवता अपने इस गिरे हुए साथी की सहायता करने के लिए समय-समय पर अपने सहृदय सहायक का परिचय देते रहते हैं।
भौतिक विज्ञान की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आदि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी के रासायनिक पदार्थों के पानी तथा सूर्य की गर्मी के साथ समन्वय होने के कारण सम्भव हुई। तब वह पानी में तैरने वाला एक जल कीटक मात्र था। उसमें जड़ पदार्थों से अपने को स्वतन्त्र करने की और आगे बढ़ने की तीन विशेषताएं थीं (1) भोजन करने और बढ़ने की शक्ति (2) घूमने-फिरने की शक्ति (3) अपने समान दूसरे प्राणी को जन्म दे सकने योग्य प्रजनन शक्ति। इनसे भी बढ़कर थी उसके ‘अहम्’ के साथ जुड़ी हुई इच्छा शक्ति।
चेतन जीव प्रेरणा को प्राणि-जगत के विकास का मूलभूत आधार माना गया। वस्तुतः यही जड़-चेतन की विभेद रेखा है। अन्यथा जड़ में भी हलचल होती है। रासायनिक अणु अपने ढंग से विकास वृद्धि और मरण परिवर्तन का क्रम चलाते हैं। अन्तर इतना ही होता है कि उनमें इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का उपयोग, अभिवर्धन एवं नियन्त्रण करने की स्वतन्त्र चेतना नहीं होती। प्रकृति प्रेरणा के वे खिलौने मात्र होते हैं। चेतन जीव में विभिन्न हलचलें तो होती ही हैं। उसमें प्रकृति प्रेरणाओं के अनुरूप अथवा प्रतिकूल चलने का स्वतन्त्र संकल्प-बल भी होता है। चेतन इसी का नाम है। जीव सत्ता का उद्गम इस चित्तशक्ति को कहा जा सकता है।
इस संसार में जीव कैसे उत्पन्न हुआ और उसका विकास किस रूप में हुआ? इस सन्दर्भ में कितनी ही मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथन यह है कि पृथ्वी में जब उष्ण गैस मात्र थी तब उसने सूर्य की परिक्रमा करते हुए जीवन तत्व का उद्भव किया था। ध्रुवों की अन्तिम सीमा को छोड़कर उसकी ऊपरी परत के नीचे यह जीवन जमा होता गया और जब जल तथा ताप का सन्तुलन हुआ तो वह जीवन नन्हें-नन्हें कृमि कीटकों के रूप में विकसित होने लगा। उसी का क्रमिक विकास वर्तमान प्राणियों के स्तर तक होता चला आया है। अभी भी विषुवत् रेखा के समीपवर्ती उष्ण प्रदेशों में जीवों की बहुलता है। इसे सूर्य और धरती की समागम स्थली कहा जाता है।
प्रो. जे.वी.एस. हाल्डेन ने अल्ट्रा वायलेट किरणों के विकरण द्वारा उच्च अणु भार वाले प्रांगारिक योगिकों का संश्लेषण होना जीवन का प्रारम्भ कारण माना है। सर आलिवर लाज का कथन है कि ईथर तत्व के साथ जीवन का अनन्त स्पन्दन अनादि काल से है। उसका आरम्भ काल वह है जब से जीवधारियों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता के रूप में उसकी अनुभूति की। जुलियन हक्सले का जड़ के विकास से चेतन की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास उपहासास्पद है। चेतना की सत्ता इस सृष्टि में अनादि काल से विद्यमान है। जड़ को वर्तमान रूप तक घसीट लाने का श्रेय उस चेतना को ही दिया जाना चाहिए।
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. हेनरी वर्गसन ने अपने ग्रन्थ ‘क्रिएटिव इवोल्यूशन’ में लिखा है। जीवन एक प्रचण्ड शक्ति है जिसने आरम्भिक ऊबड़-खाबड़ पदार्थ सम्पदा को एक व्यवस्थित और उपयोगी स्तर तक पहुंचाने का अथक प्रयत्न किया है। जार्ज वर्नार्डशा ने अपनी पुस्तक ‘मैन एण्ड सुपर मैन’ में जीवन तत्व को लाइफा फोर्स के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं जीवन सत्ता को प्रकृति की समस्त शक्तियों में सर्वोपरि स्तर की स्वतन्त्र कर्तृत्व सम्पन्न सामर्थ्य कहा जा सकता है। नैपोलियन की बात लगती तो उपहासास्पद है पर तथ्य उसमें भी है वह कहता था जीव का जन्म कीचड़ से हुआ है। कमल जैसा सुन्दर पुष्प भी तो कीचड़ में ही जन्मता है। जल, मिट्टी और ऊष्मा के संयोग से जीव की उत्पत्ति मानने वाले प्रकारान्तर से नैपोलियन की बात को ही पुष्ट करते हैं। क्या सचमुच ही हमारी आदि जन्मदात्री कीचड़ है? क्या हम कीचड़ में सने हुए जन्मे और अभी तक उस कीचड़ से उबर नहीं पाये हैं? यह एक विचित्र पहेली है, दार्शनिकों के लिए भी और भौतिक विज्ञानियों के लिए भी।
कीचड़ में से कीड़ा—कीड़े से मछली, मेढ़क, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी जीवों का उद्भव—कैसा है यह विचित्र संयोग? जिसे न स्वीकार करते बनता है और न अस्वीकार करते। प्रथम स्तनधारी ‘मैमल’ ही क्या हमारा वंश पूर्वज है? स्पीसीज वंश के स्तनपायी बनमानुष के रूप में हम विकसित हुए, और पिछली टांगों के सहारे खड़ा होना, सीधे चलना सीखा! दो हाथों को पैरों के प्रयोजन से मुक्त करके उन्हें विविध कर्म कर सकने योग्य बनाया। यह इतनी बड़ी जीवन क्रान्ति उन दिनों न जोन कितने चक्रों को पार करते हुए सम्भव हुई होगी? इस खड़े होने की प्रक्रिया ने वनमानुष और गृह मानुष के बीच बनावट का अन्तर किया है, ऐसा शरीर शास्त्री मानते हैं।
डार्विन ने अपनी पुस्तक ‘ओरिजिन आफ स्पीसीज’ में उन पुरानी मान्यताओं को झुठलाया है जिनमें यह कहा जाता रहा है कि प्रत्येक प्राणी अपने वर्तमान स्वरूप में ही अवतरित हुआ है। उन्होंने जीव के क्रमिक विकास को अपने प्रख्यात ‘विकासवाद’ दर्शन में अनेकों कारण और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है। मनुष्यों का पूर्वज वे होमोसौपियन जाति के नर-वानर को मानते हैं। एप, गुरिल्ला चिंपैंजी, आरांगओटान, गिव्वन आदि सब उसी आदि नर−वानर के वंशज हैं। उनके गोत्र ही अलग अलग हैं। मनुष्य का बाप बन्दर था, यह बात गले न उतरने पर एक बार आक्सफोर्ड के लार्ड विशप सेम्युअल विल्वर फोर्स के जीव विज्ञानी टामस हक्सले ने व्यंग पूर्वक पूछा वनमानुष आप माता के पक्ष में हैं या पिता के पक्ष में? इस पर हक्सले ने उत्तर दिया—मुझे इस बात की लज्जा नहीं कि अपने बाबा या दादी वनमानुष थे। मुझे लज्जा उन पर आती है जो अहमन्यता के कारण सचाई को पददलित करने के लिए तुले हुए हैं। उन दिनों सचमुच ही यह एक विचित्र प्रतिपादन समझा गया था कि प्राणियों ने क्रमिक विकास किया है और मनुष्य बन्दर की औलाद है। धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्रों में इस प्रतिपादन का प्रबल विरोध हुआ था। सन् 1870 में प्रशिया (जर्मनी) की सरकार ने आदेश निकाल कर प्रतिबन्ध लगा दिया था कि विकासवाद की बात किसी शिक्षा में—संस्था में न पढ़ा जाय। टिनेसी (अमेरिका) में तो एक अध्यापक पर यह मुकदमा भी चला था क्योंकि उसने छात्रों को विकासवाद के सिद्धान्त पढ़ाये।
मनुष्य और वानर की शरीर रचना में अद्भुत समानता है। इतना ही नहीं मानसिक स्तर पर भी वे दोनों बहुत कुछ मिलते हैं। शान्ति, चिन्ता, हंसी, रुदन क्रोध, उत्तेजना, विरक्ति जैसी कितनी ही सम्वेदनाएं ऐसी हैं जो मनुष्य के अतिरिक्त केवल वानरों में ही पाई जाती हैं। उनसे पारस्परिक सहयोग, स्नेह, वात्सल्य जैसी प्रवृत्तियां भी अन्य जीवों की तुलना में कहीं अधिक विकसित और स्थिर हैं।
जीव विज्ञानी मनुष्य को पंक-प्रजनन कृमि-कीटक का विकास एवं बन्दर की औलाद मानते हैं। क्या उनका प्रतिपादन मिथ्या है? दुष्प्रवृत्तियों में उसका रुझान और उत्साह देखते हुए लगता है सम्भवतः यही ठीक है कि मूलतः मानव प्राणी नर-पशु मात्र है। अन्यथा विवेकवान और दूरदर्शी होते हुए भी ऐसी गतिविधियां क्यों अपनाता जो उसके स्वयं के लिए और समस्त समाज के लिए अहितकर ही सिद्ध होती हैं।
दर्शन शास्त्री मनुष्य को गिरा हुआ देवता मानते हैं। यह निरर्थकता है? नहीं, यदि ऐसा न होता तो उसके अन्तःकरण में ऊंचा उठने और श्रेष्ठ सिद्ध होने के लिए सत्कर्म करने की ललक क्यों पाई जाती? आदर्शवादिता की, उत्कृष्टता की उमंगों का उठना और भौतिक लोभ, लिप्सा को छोड़कर परमार्थ प्रयोजनों के लिए त्याग, बलिदान का साहस जुटाना, अकारण नहीं हो सकता। परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष की हानि सहने की उमंगें उठना मानवी अन्तरात्मा की अपनी विशेषता है। यदि वह आदि काल में देव न रहा होता तो रह-रहकर वे दिव्य आकांक्षाएं उसे क्यों बेचैन किये रहती हैं? देवोपम जीवन जीने के लिए क्यों उसे कोई निरन्तर व्यथित करता रहता है?
फिर दोनों में से कौन गलत है। हम आदि में नर पशु थे या नर-नारायण? गहराई से विचार करने पर प्रतीत होता है कि शारीरिक दृष्टि से मनुष्य ने नीचे से ऊपर को प्रगति की है और आत्मिक दृष्टि से ऊपर से नीचे गिरा है। इन दिनों वे अधर में लटक रहा है। असमंजस के साथ वह एक चौराहे पर खड़ा है और सोचता है कि नर-वानर, नर-पशु, नर-कीटक बनने के लिए उसे वापिस लौटना चाहिए अथवा नर-देव बनने की दिशा में अपने चरण पीछे लौटाने चाहिए। आत्म-पक्ष कहता है (—) तुम देव थे देवत्व की ओर पीछे लौटो। देह-पक्ष कहता है कृमि कीटकों का जीवन अधिक स्वच्छन्द और निरापद है। उसी मूल उद्गम की ओर लौट कर चैन की बंशी बजानी चाहिए।
मनुष्य के उद्भव, विकास और वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में आनुवंशिक विज्ञान द्वारा भी कर्तव्य सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते रहे हैं।
आनुवंशिकता या इच्छाशक्ति—
आनुवंशिकी-विज्ञान के अन्तर्गत पिछले दिनों यह सिद्ध किया जाता रहा है कि प्राणी अपने पूर्वजों की प्रतिकृति होते हैं। माता पिता के डिम्ब-कीट और शुक्र-कीट मिल जुल कर भ्रूण-कलल में परिणत होते हैं और शरीर बनना आरम्भ हो जाता है। उस शरीर में जो मनःचेतना रहती है, उसका स्तर भी पूर्वजों की मनःस्थिति की भांति ही उत्तराधिकार में मिलता है। शरीर की संरचना और मानसिक बनावट के लिए बहुत हद तक पूर्वजों के उन जीवाणुओं को ही ठहराया गया है, जो परम्परा के रूप में वंशधरों में उतरते चले जाते हैं।
इस प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अपने आप में कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्वजों के ढांचे में ढला हुआ एक खिलौना मात्र है। यदि सन्तान को सुयोग्य सुविकसित बनाना हो तो वह कार्य पीढ़ियों पहले आरम्भ किया जाना चाहिए। अन्यथा सांचे में ढले हुए इस खिलौने में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो सकेगा। आनुवंशिकी का प्रतिपादन जहां तक मानव-प्राणी का सम्बन्ध है, बहुत ही अपूर्ण और अवास्तविक है। पशु-पक्षियों में एक हद तक यह बात सही भी हो सकती है, पर मनुष्य के लिए यह कहना अनुचित है कि वह पूर्वजों के सांचे में ढला हुआ एक उपकरण मात्र है। यह मानवी इच्छा शक्ति, विवेक-बुद्धि, स्वतन्त्र-चेतना और आत्मनिर्भरता को झुठलाना है। समाज-शास्त्री, अर्थ-शास्त्री और मनोविज्ञान वेत्ता वातावरण एवं परिस्थितियों के उत्थान पतन का कारण बताते रहे हैं। आत्म वेत्ताओं ने एक स्वर से सदा यही कहा है—मनुष्य की अन्तःचेतना स्वनिर्मित है। वह वंश परम्परा से नहीं, संचित संस्कारों और प्रस्तुत प्रयत्नों के आधार पर विकसित होती है। इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति के आधार पर अपने मानसिक ढांचे में कोई चाहे तो आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है।
आनुवंशिकी की मान्यताएं एक हद तक ही सही ठहराई जा सकती हैं। चमड़ी का रंग, चेहरा, आकृति अवयव आदि पूर्वजों की बनावट के अनुरूप हो सकते हैं, पर गुण, कर्म स्वभाव भी पूर्वजों जैसे ही हों, यह आवश्यक नहीं। यदि ऐसा हो रहा होता तो किसी कुल में सभी अच्छे और किसी कुल में सभी बुरे उत्पन्न होते। रुग्णता, स्वस्थता, बुद्धिमत्ता, सज्जनता, दुष्टता, कुशलता, अस्त-व्यस्तता भी परम्परागत होती तो प्रगतिशील वर्ग के परिवार के सभी सदस्य सुविकसित होते और पिछड़े लोगों का स्तर सदा के लिए गया-गुजरा ही बना रहता। तब उत्थान-पतन के लिए किये गये प्रयत्नों की भी कुछ सार्थकता न होती। वातावरण का भी कोई प्रभाव न पड़ता, पर ऐसी स्थिति है नहीं। पूर्वजों की स्थिति से सर्वथा भिन्न स्तर की सन्तानों के अगणित उदाहरण पग-पग पर सर्वत्र बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इससे मनुष्य की स्वतन्त्र चेतना और इच्छा-शक्ति की प्रबलता का लक्ष्य ही स्पष्ट रूप से सामने आता है।
मद्यप मनुष्यों की सन्तान क्या जन्म-जात रूप से उस लत से ग्रसित होती है? इस खोज-बीन में पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरन् उल्टा यह हुआ कि बच्चों ने बाप को मद्यपान के कारण अपनी बर्बादी करते देखा तो वे उसके विरुद्ध हो गये और उन्होंने न केवल मद्यपान से अपने को अछूता रखा, वरन् दूसरों को भी उसे अपनाने से रोका। मनुष्यों में गुण सूत्रों के हेर-फेर से जो परिणाम सामने आये हैं, उससे स्पष्ट है कि बिगाड़ने में अधिक और बनाने में कम सफलता मिली है। विकलांग और पैतृक रोगों से ग्रसित सन्तान उत्पन्न करने में आशाजनक सफलता मिली है। क्योंकि विषाक्त मारकता से भरे रसायन सदा अपना त्वरित परिणाम दिखाते हैं। यह गति विकासोन्मुख प्रयत्नों की नहीं होती। नीलाथोथा खाने से उल्टी तुरन्त हो सकती है, पर पाचन शक्ति सुधार देने के प्रयोग उतने सफल नहीं होते। देव से असुर की शक्ति को अधिक मानने का यही आधार है। मनुष्यों में मन चाही सन्तान उत्पन्न करने का प्रयोग सिर्फ इतनी मात्रा में कुछ अधिक सफल हुआ कि रंग रूप और गठन की दृष्टि से जनक-जननी का सादृश्य दृष्टिगोचर हो सके। काया की आन्तरिक दृढ़ता, बौद्धिक तीक्ष्णता एवं भावनात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने में वैज्ञानिक प्रयोगों का उत्साह-वर्धक परिणाम नहीं निकला है।
गुण सूत्रों को बदलने में इन दिनों विद्युत-ऊर्जा एवं रासायनिक हेर फेर के साधन जुटाये जा रहे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि यह बाहरी थोप-थाप स्थिर न रह सकेगी—उससे क्षणिक-चमत्कार भले ही देखा जा सके। शरीर के प्रत्येक अवयव को मस्तिष्क प्रभावित करता है और मस्तिष्क का सूत्र-संचालन इच्छा-शक्ति के हाथ में रहता है। अस्तु शारीरिक, मानसिक समस्त परिवर्तनों का तात्विक आधार इस इच्छा-शक्ति को ही मानना पड़ेगा। गुण-सूत्रों पर भी इसी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और इसी माध्यम से वह परिवर्तन किये जा सकते हैं, जो मनचाही पीढ़ियां उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिकों को अभीष्ट हैं।
अभीष्ट स्तर की पीढ़ियां क्या रासायनिक हेर-फेर अथवा विद्युतीय प्रयोग उपकरणों द्वारा प्रयोगशालाओं में विनिर्मित हो सकती हैं। यह एक जटिल प्रश्न है। यदि ऐसा हो सका तो यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य इच्छा-शक्ति का धनी नहीं, वरन् रासायनिक पदार्थों की परावलम्बी प्रतिक्रिया मात्र है। यदि यह सिद्ध हो सका तो इसे मनोबल और आत्मबल की गरिमा समाप्त कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जायगा, पर ऐसा हो सकना सम्भव दिखाई नहीं पड़ता—भले ही उसके लिए एड़ी-चोटी प्रयत्न कितने ही किये जाते रहें।
शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव डाले जाते रहे हैं, पर प्राणी की मूल इच्छा ने उस दबाव को आवश्यक नहीं समझा तो उस तरह के परिवर्तन नहीं हो सके। चीन में शताब्दियों तक स्त्रियों के पैर छोटे होना—सौन्दर्य का चिन्ह माना गया, इसके लिए उन्हें कड़े जूते पहनाये जाते थे। उससे पैर छोटे बनाने में सफलता मिली। पर वंश-परम्परा की दृष्टि से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हर नई लड़की के पैर पूरे अनुपात से ही होते थे।
प्राणियों के क्रमिक-विकास में इच्छा-शक्ति का ही प्रधान स्थान रहा है। मनुष्य तो मनोबल का धनी है, उसकी बात जाने भी दें और अन्य प्राणधारियों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि उनकी वंश-परम्परा में बहुमुखी परिवर्तन होता रहा है। इसका कारण सामयिक परिस्थितियों का चेतना पर पड़ने वाला दबाव ही प्रधान कारण रहा है। असुविधाओं को हटाने और सुविधाएं बढ़ाने की आन्तरिक आकांक्षा ने प्राणियों की शारीरिक स्थिति और आकृति में ही नहीं प्रकृति में भी भारी हेर-फेर प्रस्तुत किया है। जीव-विज्ञानी इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं।
यदि पूर्वजों के गुण लेकर ही सन्तानें उत्पन्न होने वाली बात को सही माना जाय तो जीवों की आकृति-प्रकृति में परिवर्तन कैसे सम्भव हुआ? उस स्थिति में तो पीढ़ियों का स्तर एक ही प्रकार का चलता रहना चाहिए था।
लेमार्क ने प्राणियों का स्तर बदलने में वातावरण को, परिस्थितियों को श्रेय दिया है। वे कहते हैं—इच्छा-शक्ति इन्हीं दबावों के कारण उभरती उतरती है। सुविधा-सम्पन्न परिस्थितियों के प्राणियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। अतएव उनका शरीर ही नहीं, बुद्धि-कौशल भी ठप्प पड़ता जाता है। अमीरी के वैभव में पले हुए लोग अक्सर छुई मुई बने रह जाते हैं और उनका चरखा बखेर देने के लिए एक छोटा-सा आघात ही पर्याप्त होता है।
लेमार्क ने नये किस्म के अनेक जीवधारियों की उत्पत्ति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बाहर से मौलिक जीवन दीखने पर भी वस्तुतः किसी ऐसे पूर्व प्राणी के ही वंशज होते हैं, जिन्हें परिस्थितियों के दबाव से अपने परम्परागत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा।
जीवों के विकास-इतिहास के पन्ने-पन्ने पर यह प्रमाण भरे पड़े हैं कि प्राणियों के अंग प्रत्येक निष्क्रियता के आधार पर कुण्ठित हुए हैं और सक्रियता ने उन्हें विकसित किया है। प्रवृत्ति, प्रयोजन और चेष्टाओं का मूल इच्छा-शक्ति ही है। असल में यह इच्छाशक्ति ही प्राणिसत्ता में विकास, अवसाद उत्पन्न करती है। रासायनिक पदार्थों और गुण-सूत्रों की वंश-परम्परा विज्ञान में कायिक क्षमता को एक अंश तक प्रभावित करने वाला आधार भर माना जाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान-वेत्ता मौलिक-भूल यह कर रहे हैं कि मानवी-सत्ता को उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र समझा है और उसका विकास करने के लिए जनक-जननी को-उनके जनन-रसों को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। इस एकांगी आधार को लेकर मनचाही आकृति-प्रकृति की पीढ़ियां वे कदाचित ही पैदा कर सकें।
वैज्ञानिक बीजमन ने चूहों और चुहियों की लगातार बीस पीढ़ियां तक पूछें काटीं और देखा कि क्या इसके फल स्वरूप बिना पूंछ वाले चूहे पैदा किये जा सकते हैं? उन्हें अपने प्रयोग में सर्वथा असफल होना पड़ा। बिना पूंछ के मां बाप भी पूंछ वाले बच्चे ही जनते चले गये। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मात्र शारीरिक हेर फेर से वंशानुक्रम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए प्राणी की अपनी रुचि एवं इच्छा का समावेश होना नितान्त आवश्यक है।
हर्वर्ट स्पेन्सर ने अपनी खोजें में ऐसे कितने ही प्राणियों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिन्होंने शरीर के किसी अवयव को निष्क्रिय रखा तो वह क्षीण होता चला गया और लुप्त भी हो गया। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं, जिनमें ‘‘आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है’’ वाले सिद्धान्त को सही सिद्ध करते हुए अपने शरीर में कई तरह के नये पुर्जे विकसित किये पुरानों को आश्चर्यजनक स्तर तक परिष्कृत किया।
समुद्र-तट की गहराई में रहने वाली मछलियों को प्रकाश से वंचित रहना पड़ता है। अतएव उनकी आंखों का चिन्ह रहते हुए भी उनमें रोशनी नहीं होती है। आंख वाले अन्धों में उनकी गणना की जा सकती है। अंधेरी गुफाओं में जन्मने और पलने वाले थलचरों का भी यही हाल होता है। उनकी आंखें ऐसी होती है, जो अन्धेरे में ही कुछ काम कर सके। प्रकाश में वे बेतरह चौंधिया जाती हैं और निकम्मी साबित होती हैं।
समर्थ का चुनाव मात्र शारीरिक बलिष्ठता पर निर्भर नहीं है, वरन् सच पूछा जाय तो उनकी मनःस्थिति की ही परख इस कसौटी पर होती है। पशुवर्ग और सरीसृप वर्ग के विशाल-काय प्राणी आदिम काल में थे। उनकी शरीरगत क्षमता अद्भुत थी, फिर भी वे मन्द-बुद्धि, अदूरदर्शिता, आलस जैसी कमियों के कारण दुर्बल संज्ञा वाले ही सिद्ध हुए और अपना अस्तित्व खो बैठे। जब कि उसी समय में छोटी काया वाले प्राणी अपने मनोबल के कारण न केवल अपनी सत्ता संभालते रहे वरन् क्रमशः विकासोन्मुख भी होते चले गये।
जीवों के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि उन्हें परिस्थितियों से जूझना पड़ा-अवरोध के सामने टिके रहने के लिए अपने शरीर में तथा स्वभाव में अन्तर करना पड़ा। यह परिवर्तन किसी रासायनिक हेर-फेर के कारण नहीं, विशुद्ध रूप से इच्छा-शक्ति की प्रवाह-धारा बदल जाने से ही सम्भव हुआ है। जीवन संग्राम में जूझने की पुरुषार्थ-परायणता का उपहार ही अल्प-प्राण जीवों को महाप्राण स्तर का बन सकने के रूप में मिला है। जिन्होंने विपत्ति से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी और हताश होकर पैर पसार बैठे, उन्हें प्रकृति ने कूड़े कचरे की तरह बुहार कर घूरे पर पटक दिया। किसान और माली भी तो अपने खेत बाग में अनुपयोगी खर-पतवार की ऐसी ही उखाड़-पछाड़ करते रहते हैं। विकास की उपलब्धि पूर्णतया जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप ही मिलती है और इस संघर्षशीलता का पूरा आधार साहसी एवं पुरुषार्थी मनोभूमि के साथ जुड़ता रहता है।
आनुवंशिकी विज्ञान की अन्यान्य शोधें कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों, पर यह प्रतिपादन तथ्य व तर्क किसी भी कसौटी पर स्वीकार्य नहीं हो सकता कि प्राणियों का स्तर पूर्वजों के परम्परागत गुण सूत्रों पर निर्भर करता है। विशेषतः मनुष्य का स्तर तो परम्परागत सूत्रों पर किसी भी प्रकार पूरी तरह निर्भर नहीं करता है। परमात्मा ने मनुष्य में बीज रूप से वे सारी विशेषतायें भरदी हैं जिनके द्वारा इच्छाशक्ति की प्रचंड समर्थता के आधार पर शारीरिक मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सम्पन्न कर ले। इन सम्भावनाओं को मान्यता देने के उपरान्त ही वंशगत विशेषताओं की चर्चा की जाय, यही उचित है।
आदम और हव्वा स्वर्ग में रहते थे उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अभक्ष्य खाया और जमीन पर आ गिरे। उनके वंशज मनुष्य कहलाए। देवता और अवतारों का धरती पर उतर का मनुष्य शरीर धारण करना और सन्तानोत्पादन में संलग्न होना। प्रायः इसी से मिलती जुलती कथा गाथाएं समस्त धर्मों में प्रचलित हैं, जिनमें आदि मानव के अस्तित्व का आरम्भ किस प्रकार हुआ, इस जिज्ञासा का समाधान किया गया है। यह मान्यताएं बताती हैं कि मनुष्य गिरा हुआ देवता है। स्वर्ग लोक के देवता अपने इस गिरे हुए साथी की सहायता करने के लिए समय-समय पर अपने सहृदय सहायक का परिचय देते रहते हैं।
भौतिक विज्ञान की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आदि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी के रासायनिक पदार्थों के पानी तथा सूर्य की गर्मी के साथ समन्वय होने के कारण सम्भव हुई। तब वह पानी में तैरने वाला एक जल कीटक मात्र था। उसमें जड़ पदार्थों से अपने को स्वतन्त्र करने की और आगे बढ़ने की तीन विशेषताएं थीं (1) भोजन करने और बढ़ने की शक्ति (2) घूमने-फिरने की शक्ति (3) अपने समान दूसरे प्राणी को जन्म दे सकने योग्य प्रजनन शक्ति। इनसे भी बढ़कर थी उसके ‘अहम्’ के साथ जुड़ी हुई इच्छा शक्ति।
चेतन जीव प्रेरणा को प्राणि-जगत के विकास का मूलभूत आधार माना गया। वस्तुतः यही जड़-चेतन की विभेद रेखा है। अन्यथा जड़ में भी हलचल होती है। रासायनिक अणु अपने ढंग से विकास वृद्धि और मरण परिवर्तन का क्रम चलाते हैं। अन्तर इतना ही होता है कि उनमें इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का उपयोग, अभिवर्धन एवं नियन्त्रण करने की स्वतन्त्र चेतना नहीं होती। प्रकृति प्रेरणा के वे खिलौने मात्र होते हैं। चेतन जीव में विभिन्न हलचलें तो होती ही हैं। उसमें प्रकृति प्रेरणाओं के अनुरूप अथवा प्रतिकूल चलने का स्वतन्त्र संकल्प-बल भी होता है। चेतन इसी का नाम है। जीव सत्ता का उद्गम इस चित्तशक्ति को कहा जा सकता है।
इस संसार में जीव कैसे उत्पन्न हुआ और उसका विकास किस रूप में हुआ? इस सन्दर्भ में कितनी ही मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथन यह है कि पृथ्वी में जब उष्ण गैस मात्र थी तब उसने सूर्य की परिक्रमा करते हुए जीवन तत्व का उद्भव किया था। ध्रुवों की अन्तिम सीमा को छोड़कर उसकी ऊपरी परत के नीचे यह जीवन जमा होता गया और जब जल तथा ताप का सन्तुलन हुआ तो वह जीवन नन्हें-नन्हें कृमि कीटकों के रूप में विकसित होने लगा। उसी का क्रमिक विकास वर्तमान प्राणियों के स्तर तक होता चला आया है। अभी भी विषुवत् रेखा के समीपवर्ती उष्ण प्रदेशों में जीवों की बहुलता है। इसे सूर्य और धरती की समागम स्थली कहा जाता है।
प्रो. जे.वी.एस. हाल्डेन ने अल्ट्रा वायलेट किरणों के विकरण द्वारा उच्च अणु भार वाले प्रांगारिक योगिकों का संश्लेषण होना जीवन का प्रारम्भ कारण माना है। सर आलिवर लाज का कथन है कि ईथर तत्व के साथ जीवन का अनन्त स्पन्दन अनादि काल से है। उसका आरम्भ काल वह है जब से जीवधारियों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता के रूप में उसकी अनुभूति की। जुलियन हक्सले का जड़ के विकास से चेतन की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास उपहासास्पद है। चेतना की सत्ता इस सृष्टि में अनादि काल से विद्यमान है। जड़ को वर्तमान रूप तक घसीट लाने का श्रेय उस चेतना को ही दिया जाना चाहिए।
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. हेनरी वर्गसन ने अपने ग्रन्थ ‘क्रिएटिव इवोल्यूशन’ में लिखा है। जीवन एक प्रचण्ड शक्ति है जिसने आरम्भिक ऊबड़-खाबड़ पदार्थ सम्पदा को एक व्यवस्थित और उपयोगी स्तर तक पहुंचाने का अथक प्रयत्न किया है। जार्ज वर्नार्डशा ने अपनी पुस्तक ‘मैन एण्ड सुपर मैन’ में जीवन तत्व को लाइफा फोर्स के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं जीवन सत्ता को प्रकृति की समस्त शक्तियों में सर्वोपरि स्तर की स्वतन्त्र कर्तृत्व सम्पन्न सामर्थ्य कहा जा सकता है। नैपोलियन की बात लगती तो उपहासास्पद है पर तथ्य उसमें भी है वह कहता था जीव का जन्म कीचड़ से हुआ है। कमल जैसा सुन्दर पुष्प भी तो कीचड़ में ही जन्मता है। जल, मिट्टी और ऊष्मा के संयोग से जीव की उत्पत्ति मानने वाले प्रकारान्तर से नैपोलियन की बात को ही पुष्ट करते हैं। क्या सचमुच ही हमारी आदि जन्मदात्री कीचड़ है? क्या हम कीचड़ में सने हुए जन्मे और अभी तक उस कीचड़ से उबर नहीं पाये हैं? यह एक विचित्र पहेली है, दार्शनिकों के लिए भी और भौतिक विज्ञानियों के लिए भी।
कीचड़ में से कीड़ा—कीड़े से मछली, मेढ़क, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी जीवों का उद्भव—कैसा है यह विचित्र संयोग? जिसे न स्वीकार करते बनता है और न अस्वीकार करते। प्रथम स्तनधारी ‘मैमल’ ही क्या हमारा वंश पूर्वज है? स्पीसीज वंश के स्तनपायी बनमानुष के रूप में हम विकसित हुए, और पिछली टांगों के सहारे खड़ा होना, सीधे चलना सीखा! दो हाथों को पैरों के प्रयोजन से मुक्त करके उन्हें विविध कर्म कर सकने योग्य बनाया। यह इतनी बड़ी जीवन क्रान्ति उन दिनों न जोन कितने चक्रों को पार करते हुए सम्भव हुई होगी? इस खड़े होने की प्रक्रिया ने वनमानुष और गृह मानुष के बीच बनावट का अन्तर किया है, ऐसा शरीर शास्त्री मानते हैं।
डार्विन ने अपनी पुस्तक ‘ओरिजिन आफ स्पीसीज’ में उन पुरानी मान्यताओं को झुठलाया है जिनमें यह कहा जाता रहा है कि प्रत्येक प्राणी अपने वर्तमान स्वरूप में ही अवतरित हुआ है। उन्होंने जीव के क्रमिक विकास को अपने प्रख्यात ‘विकासवाद’ दर्शन में अनेकों कारण और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है। मनुष्यों का पूर्वज वे होमोसौपियन जाति के नर-वानर को मानते हैं। एप, गुरिल्ला चिंपैंजी, आरांगओटान, गिव्वन आदि सब उसी आदि नर−वानर के वंशज हैं। उनके गोत्र ही अलग अलग हैं। मनुष्य का बाप बन्दर था, यह बात गले न उतरने पर एक बार आक्सफोर्ड के लार्ड विशप सेम्युअल विल्वर फोर्स के जीव विज्ञानी टामस हक्सले ने व्यंग पूर्वक पूछा वनमानुष आप माता के पक्ष में हैं या पिता के पक्ष में? इस पर हक्सले ने उत्तर दिया—मुझे इस बात की लज्जा नहीं कि अपने बाबा या दादी वनमानुष थे। मुझे लज्जा उन पर आती है जो अहमन्यता के कारण सचाई को पददलित करने के लिए तुले हुए हैं। उन दिनों सचमुच ही यह एक विचित्र प्रतिपादन समझा गया था कि प्राणियों ने क्रमिक विकास किया है और मनुष्य बन्दर की औलाद है। धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्रों में इस प्रतिपादन का प्रबल विरोध हुआ था। सन् 1870 में प्रशिया (जर्मनी) की सरकार ने आदेश निकाल कर प्रतिबन्ध लगा दिया था कि विकासवाद की बात किसी शिक्षा में—संस्था में न पढ़ा जाय। टिनेसी (अमेरिका) में तो एक अध्यापक पर यह मुकदमा भी चला था क्योंकि उसने छात्रों को विकासवाद के सिद्धान्त पढ़ाये।
मनुष्य और वानर की शरीर रचना में अद्भुत समानता है। इतना ही नहीं मानसिक स्तर पर भी वे दोनों बहुत कुछ मिलते हैं। शान्ति, चिन्ता, हंसी, रुदन क्रोध, उत्तेजना, विरक्ति जैसी कितनी ही सम्वेदनाएं ऐसी हैं जो मनुष्य के अतिरिक्त केवल वानरों में ही पाई जाती हैं। उनसे पारस्परिक सहयोग, स्नेह, वात्सल्य जैसी प्रवृत्तियां भी अन्य जीवों की तुलना में कहीं अधिक विकसित और स्थिर हैं।
जीव विज्ञानी मनुष्य को पंक-प्रजनन कृमि-कीटक का विकास एवं बन्दर की औलाद मानते हैं। क्या उनका प्रतिपादन मिथ्या है? दुष्प्रवृत्तियों में उसका रुझान और उत्साह देखते हुए लगता है सम्भवतः यही ठीक है कि मूलतः मानव प्राणी नर-पशु मात्र है। अन्यथा विवेकवान और दूरदर्शी होते हुए भी ऐसी गतिविधियां क्यों अपनाता जो उसके स्वयं के लिए और समस्त समाज के लिए अहितकर ही सिद्ध होती हैं।
दर्शन शास्त्री मनुष्य को गिरा हुआ देवता मानते हैं। यह निरर्थकता है? नहीं, यदि ऐसा न होता तो उसके अन्तःकरण में ऊंचा उठने और श्रेष्ठ सिद्ध होने के लिए सत्कर्म करने की ललक क्यों पाई जाती? आदर्शवादिता की, उत्कृष्टता की उमंगों का उठना और भौतिक लोभ, लिप्सा को छोड़कर परमार्थ प्रयोजनों के लिए त्याग, बलिदान का साहस जुटाना, अकारण नहीं हो सकता। परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष की हानि सहने की उमंगें उठना मानवी अन्तरात्मा की अपनी विशेषता है। यदि वह आदि काल में देव न रहा होता तो रह-रहकर वे दिव्य आकांक्षाएं उसे क्यों बेचैन किये रहती हैं? देवोपम जीवन जीने के लिए क्यों उसे कोई निरन्तर व्यथित करता रहता है?
फिर दोनों में से कौन गलत है। हम आदि में नर पशु थे या नर-नारायण? गहराई से विचार करने पर प्रतीत होता है कि शारीरिक दृष्टि से मनुष्य ने नीचे से ऊपर को प्रगति की है और आत्मिक दृष्टि से ऊपर से नीचे गिरा है। इन दिनों वे अधर में लटक रहा है। असमंजस के साथ वह एक चौराहे पर खड़ा है और सोचता है कि नर-वानर, नर-पशु, नर-कीटक बनने के लिए उसे वापिस लौटना चाहिए अथवा नर-देव बनने की दिशा में अपने चरण पीछे लौटाने चाहिए। आत्म-पक्ष कहता है (—) तुम देव थे देवत्व की ओर पीछे लौटो। देह-पक्ष कहता है कृमि कीटकों का जीवन अधिक स्वच्छन्द और निरापद है। उसी मूल उद्गम की ओर लौट कर चैन की बंशी बजानी चाहिए।
मनुष्य के उद्भव, विकास और वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में आनुवंशिक विज्ञान द्वारा भी कर्तव्य सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते रहे हैं।
आनुवंशिकता या इच्छाशक्ति—
आनुवंशिकी-विज्ञान के अन्तर्गत पिछले दिनों यह सिद्ध किया जाता रहा है कि प्राणी अपने पूर्वजों की प्रतिकृति होते हैं। माता पिता के डिम्ब-कीट और शुक्र-कीट मिल जुल कर भ्रूण-कलल में परिणत होते हैं और शरीर बनना आरम्भ हो जाता है। उस शरीर में जो मनःचेतना रहती है, उसका स्तर भी पूर्वजों की मनःस्थिति की भांति ही उत्तराधिकार में मिलता है। शरीर की संरचना और मानसिक बनावट के लिए बहुत हद तक पूर्वजों के उन जीवाणुओं को ही ठहराया गया है, जो परम्परा के रूप में वंशधरों में उतरते चले जाते हैं।
इस प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अपने आप में कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्वजों के ढांचे में ढला हुआ एक खिलौना मात्र है। यदि सन्तान को सुयोग्य सुविकसित बनाना हो तो वह कार्य पीढ़ियों पहले आरम्भ किया जाना चाहिए। अन्यथा सांचे में ढले हुए इस खिलौने में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो सकेगा। आनुवंशिकी का प्रतिपादन जहां तक मानव-प्राणी का सम्बन्ध है, बहुत ही अपूर्ण और अवास्तविक है। पशु-पक्षियों में एक हद तक यह बात सही भी हो सकती है, पर मनुष्य के लिए यह कहना अनुचित है कि वह पूर्वजों के सांचे में ढला हुआ एक उपकरण मात्र है। यह मानवी इच्छा शक्ति, विवेक-बुद्धि, स्वतन्त्र-चेतना और आत्मनिर्भरता को झुठलाना है। समाज-शास्त्री, अर्थ-शास्त्री और मनोविज्ञान वेत्ता वातावरण एवं परिस्थितियों के उत्थान पतन का कारण बताते रहे हैं। आत्म वेत्ताओं ने एक स्वर से सदा यही कहा है—मनुष्य की अन्तःचेतना स्वनिर्मित है। वह वंश परम्परा से नहीं, संचित संस्कारों और प्रस्तुत प्रयत्नों के आधार पर विकसित होती है। इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति के आधार पर अपने मानसिक ढांचे में कोई चाहे तो आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है।
आनुवंशिकी की मान्यताएं एक हद तक ही सही ठहराई जा सकती हैं। चमड़ी का रंग, चेहरा, आकृति अवयव आदि पूर्वजों की बनावट के अनुरूप हो सकते हैं, पर गुण, कर्म स्वभाव भी पूर्वजों जैसे ही हों, यह आवश्यक नहीं। यदि ऐसा हो रहा होता तो किसी कुल में सभी अच्छे और किसी कुल में सभी बुरे उत्पन्न होते। रुग्णता, स्वस्थता, बुद्धिमत्ता, सज्जनता, दुष्टता, कुशलता, अस्त-व्यस्तता भी परम्परागत होती तो प्रगतिशील वर्ग के परिवार के सभी सदस्य सुविकसित होते और पिछड़े लोगों का स्तर सदा के लिए गया-गुजरा ही बना रहता। तब उत्थान-पतन के लिए किये गये प्रयत्नों की भी कुछ सार्थकता न होती। वातावरण का भी कोई प्रभाव न पड़ता, पर ऐसी स्थिति है नहीं। पूर्वजों की स्थिति से सर्वथा भिन्न स्तर की सन्तानों के अगणित उदाहरण पग-पग पर सर्वत्र बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इससे मनुष्य की स्वतन्त्र चेतना और इच्छा-शक्ति की प्रबलता का लक्ष्य ही स्पष्ट रूप से सामने आता है।
मद्यप मनुष्यों की सन्तान क्या जन्म-जात रूप से उस लत से ग्रसित होती है? इस खोज-बीन में पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरन् उल्टा यह हुआ कि बच्चों ने बाप को मद्यपान के कारण अपनी बर्बादी करते देखा तो वे उसके विरुद्ध हो गये और उन्होंने न केवल मद्यपान से अपने को अछूता रखा, वरन् दूसरों को भी उसे अपनाने से रोका। मनुष्यों में गुण सूत्रों के हेर-फेर से जो परिणाम सामने आये हैं, उससे स्पष्ट है कि बिगाड़ने में अधिक और बनाने में कम सफलता मिली है। विकलांग और पैतृक रोगों से ग्रसित सन्तान उत्पन्न करने में आशाजनक सफलता मिली है। क्योंकि विषाक्त मारकता से भरे रसायन सदा अपना त्वरित परिणाम दिखाते हैं। यह गति विकासोन्मुख प्रयत्नों की नहीं होती। नीलाथोथा खाने से उल्टी तुरन्त हो सकती है, पर पाचन शक्ति सुधार देने के प्रयोग उतने सफल नहीं होते। देव से असुर की शक्ति को अधिक मानने का यही आधार है। मनुष्यों में मन चाही सन्तान उत्पन्न करने का प्रयोग सिर्फ इतनी मात्रा में कुछ अधिक सफल हुआ कि रंग रूप और गठन की दृष्टि से जनक-जननी का सादृश्य दृष्टिगोचर हो सके। काया की आन्तरिक दृढ़ता, बौद्धिक तीक्ष्णता एवं भावनात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने में वैज्ञानिक प्रयोगों का उत्साह-वर्धक परिणाम नहीं निकला है।
गुण सूत्रों को बदलने में इन दिनों विद्युत-ऊर्जा एवं रासायनिक हेर फेर के साधन जुटाये जा रहे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि यह बाहरी थोप-थाप स्थिर न रह सकेगी—उससे क्षणिक-चमत्कार भले ही देखा जा सके। शरीर के प्रत्येक अवयव को मस्तिष्क प्रभावित करता है और मस्तिष्क का सूत्र-संचालन इच्छा-शक्ति के हाथ में रहता है। अस्तु शारीरिक, मानसिक समस्त परिवर्तनों का तात्विक आधार इस इच्छा-शक्ति को ही मानना पड़ेगा। गुण-सूत्रों पर भी इसी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और इसी माध्यम से वह परिवर्तन किये जा सकते हैं, जो मनचाही पीढ़ियां उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिकों को अभीष्ट हैं।
अभीष्ट स्तर की पीढ़ियां क्या रासायनिक हेर-फेर अथवा विद्युतीय प्रयोग उपकरणों द्वारा प्रयोगशालाओं में विनिर्मित हो सकती हैं। यह एक जटिल प्रश्न है। यदि ऐसा हो सका तो यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य इच्छा-शक्ति का धनी नहीं, वरन् रासायनिक पदार्थों की परावलम्बी प्रतिक्रिया मात्र है। यदि यह सिद्ध हो सका तो इसे मनोबल और आत्मबल की गरिमा समाप्त कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जायगा, पर ऐसा हो सकना सम्भव दिखाई नहीं पड़ता—भले ही उसके लिए एड़ी-चोटी प्रयत्न कितने ही किये जाते रहें।
शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव डाले जाते रहे हैं, पर प्राणी की मूल इच्छा ने उस दबाव को आवश्यक नहीं समझा तो उस तरह के परिवर्तन नहीं हो सके। चीन में शताब्दियों तक स्त्रियों के पैर छोटे होना—सौन्दर्य का चिन्ह माना गया, इसके लिए उन्हें कड़े जूते पहनाये जाते थे। उससे पैर छोटे बनाने में सफलता मिली। पर वंश-परम्परा की दृष्टि से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हर नई लड़की के पैर पूरे अनुपात से ही होते थे।
प्राणियों के क्रमिक-विकास में इच्छा-शक्ति का ही प्रधान स्थान रहा है। मनुष्य तो मनोबल का धनी है, उसकी बात जाने भी दें और अन्य प्राणधारियों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि उनकी वंश-परम्परा में बहुमुखी परिवर्तन होता रहा है। इसका कारण सामयिक परिस्थितियों का चेतना पर पड़ने वाला दबाव ही प्रधान कारण रहा है। असुविधाओं को हटाने और सुविधाएं बढ़ाने की आन्तरिक आकांक्षा ने प्राणियों की शारीरिक स्थिति और आकृति में ही नहीं प्रकृति में भी भारी हेर-फेर प्रस्तुत किया है। जीव-विज्ञानी इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं।
यदि पूर्वजों के गुण लेकर ही सन्तानें उत्पन्न होने वाली बात को सही माना जाय तो जीवों की आकृति-प्रकृति में परिवर्तन कैसे सम्भव हुआ? उस स्थिति में तो पीढ़ियों का स्तर एक ही प्रकार का चलता रहना चाहिए था।
लेमार्क ने प्राणियों का स्तर बदलने में वातावरण को, परिस्थितियों को श्रेय दिया है। वे कहते हैं—इच्छा-शक्ति इन्हीं दबावों के कारण उभरती उतरती है। सुविधा-सम्पन्न परिस्थितियों के प्राणियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। अतएव उनका शरीर ही नहीं, बुद्धि-कौशल भी ठप्प पड़ता जाता है। अमीरी के वैभव में पले हुए लोग अक्सर छुई मुई बने रह जाते हैं और उनका चरखा बखेर देने के लिए एक छोटा-सा आघात ही पर्याप्त होता है।
लेमार्क ने नये किस्म के अनेक जीवधारियों की उत्पत्ति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बाहर से मौलिक जीवन दीखने पर भी वस्तुतः किसी ऐसे पूर्व प्राणी के ही वंशज होते हैं, जिन्हें परिस्थितियों के दबाव से अपने परम्परागत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा।
जीवों के विकास-इतिहास के पन्ने-पन्ने पर यह प्रमाण भरे पड़े हैं कि प्राणियों के अंग प्रत्येक निष्क्रियता के आधार पर कुण्ठित हुए हैं और सक्रियता ने उन्हें विकसित किया है। प्रवृत्ति, प्रयोजन और चेष्टाओं का मूल इच्छा-शक्ति ही है। असल में यह इच्छाशक्ति ही प्राणिसत्ता में विकास, अवसाद उत्पन्न करती है। रासायनिक पदार्थों और गुण-सूत्रों की वंश-परम्परा विज्ञान में कायिक क्षमता को एक अंश तक प्रभावित करने वाला आधार भर माना जाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान-वेत्ता मौलिक-भूल यह कर रहे हैं कि मानवी-सत्ता को उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र समझा है और उसका विकास करने के लिए जनक-जननी को-उनके जनन-रसों को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। इस एकांगी आधार को लेकर मनचाही आकृति-प्रकृति की पीढ़ियां वे कदाचित ही पैदा कर सकें।
वैज्ञानिक बीजमन ने चूहों और चुहियों की लगातार बीस पीढ़ियां तक पूछें काटीं और देखा कि क्या इसके फल स्वरूप बिना पूंछ वाले चूहे पैदा किये जा सकते हैं? उन्हें अपने प्रयोग में सर्वथा असफल होना पड़ा। बिना पूंछ के मां बाप भी पूंछ वाले बच्चे ही जनते चले गये। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मात्र शारीरिक हेर फेर से वंशानुक्रम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए प्राणी की अपनी रुचि एवं इच्छा का समावेश होना नितान्त आवश्यक है।
हर्वर्ट स्पेन्सर ने अपनी खोजें में ऐसे कितने ही प्राणियों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिन्होंने शरीर के किसी अवयव को निष्क्रिय रखा तो वह क्षीण होता चला गया और लुप्त भी हो गया। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं, जिनमें ‘‘आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है’’ वाले सिद्धान्त को सही सिद्ध करते हुए अपने शरीर में कई तरह के नये पुर्जे विकसित किये पुरानों को आश्चर्यजनक स्तर तक परिष्कृत किया।
समुद्र-तट की गहराई में रहने वाली मछलियों को प्रकाश से वंचित रहना पड़ता है। अतएव उनकी आंखों का चिन्ह रहते हुए भी उनमें रोशनी नहीं होती है। आंख वाले अन्धों में उनकी गणना की जा सकती है। अंधेरी गुफाओं में जन्मने और पलने वाले थलचरों का भी यही हाल होता है। उनकी आंखें ऐसी होती है, जो अन्धेरे में ही कुछ काम कर सके। प्रकाश में वे बेतरह चौंधिया जाती हैं और निकम्मी साबित होती हैं।
समर्थ का चुनाव मात्र शारीरिक बलिष्ठता पर निर्भर नहीं है, वरन् सच पूछा जाय तो उनकी मनःस्थिति की ही परख इस कसौटी पर होती है। पशुवर्ग और सरीसृप वर्ग के विशाल-काय प्राणी आदिम काल में थे। उनकी शरीरगत क्षमता अद्भुत थी, फिर भी वे मन्द-बुद्धि, अदूरदर्शिता, आलस जैसी कमियों के कारण दुर्बल संज्ञा वाले ही सिद्ध हुए और अपना अस्तित्व खो बैठे। जब कि उसी समय में छोटी काया वाले प्राणी अपने मनोबल के कारण न केवल अपनी सत्ता संभालते रहे वरन् क्रमशः विकासोन्मुख भी होते चले गये।
जीवों के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि उन्हें परिस्थितियों से जूझना पड़ा-अवरोध के सामने टिके रहने के लिए अपने शरीर में तथा स्वभाव में अन्तर करना पड़ा। यह परिवर्तन किसी रासायनिक हेर-फेर के कारण नहीं, विशुद्ध रूप से इच्छा-शक्ति की प्रवाह-धारा बदल जाने से ही सम्भव हुआ है। जीवन संग्राम में जूझने की पुरुषार्थ-परायणता का उपहार ही अल्प-प्राण जीवों को महाप्राण स्तर का बन सकने के रूप में मिला है। जिन्होंने विपत्ति से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी और हताश होकर पैर पसार बैठे, उन्हें प्रकृति ने कूड़े कचरे की तरह बुहार कर घूरे पर पटक दिया। किसान और माली भी तो अपने खेत बाग में अनुपयोगी खर-पतवार की ऐसी ही उखाड़-पछाड़ करते रहते हैं। विकास की उपलब्धि पूर्णतया जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप ही मिलती है और इस संघर्षशीलता का पूरा आधार साहसी एवं पुरुषार्थी मनोभूमि के साथ जुड़ता रहता है।
आनुवंशिकी विज्ञान की अन्यान्य शोधें कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों, पर यह प्रतिपादन तथ्य व तर्क किसी भी कसौटी पर स्वीकार्य नहीं हो सकता कि प्राणियों का स्तर पूर्वजों के परम्परागत गुण सूत्रों पर निर्भर करता है। विशेषतः मनुष्य का स्तर तो परम्परागत सूत्रों पर किसी भी प्रकार पूरी तरह निर्भर नहीं करता है। परमात्मा ने मनुष्य में बीज रूप से वे सारी विशेषतायें भरदी हैं जिनके द्वारा इच्छाशक्ति की प्रचंड समर्थता के आधार पर शारीरिक मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सम्पन्न कर ले। इन सम्भावनाओं को मान्यता देने के उपरान्त ही वंशगत विशेषताओं की चर्चा की जाय, यही उचित है।