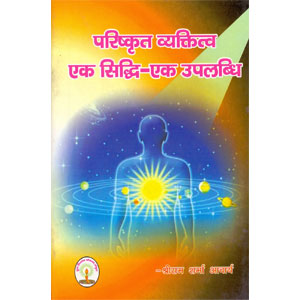परिष्कृत व्यक्तित्व-एक सिद्धि, एक उपलब्धि 
उत्थान की आकांक्षा और दिशाधारा
Read Scan Version
प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहना जीवधारी की एक स्वाभाविक वृत्ति है। जीवन के आरंभ से अब तक प्रगति का यदि लेखा-जोखा लिया जाय तो यही तथ्य अधिकाधिक उजागर होता है। अमीबा जीवन का आदि स्वरूप माना जाता रहा है। एक कोशीय जीवधारी इस प्रकृति के घटक ने क्रमिक विकास करते-करते कई-कई इन्द्रियां और काया की कई-कई इकाइयां विकसित की हैं। यह सब अनायास ही संभव नहीं हो गया, इसके लिए प्राणियों की इच्छा-शक्ति ने, अन्तःचेतना एवं स्फुरणा ने असाधारण भूमिका निभाई है। वस्तुतः यह उनका चेतनात्मक पुरुषार्थ है जिससे उनकी जैविक क्षमताओं का विकास हुआ है।
प्रकृति ने जीवधारियों के निर्वाह की सुविधा स्वेच्छापूर्वक प्रदान की है। ऐसा न होता तो जीवन के लिए अपना अस्तित्व बनाये रहना, अपनी प्रगति के साधन-सामग्री उपलब्ध कर सकना ही संभव न होता, तब उन्नति करने और समग्र-समर्थ होने की बात ही कैसे बनती? इतने पर भी यह मानकर चलना होगा कि जीवधारी का अपना निजी स्वभाव अग्रगमन के लिए, अभ्युदय के लिए अनवरत पुरुषार्थ करना है। इसी को इच्छा, अभिलाषा और आकांक्षा कहते हैं, इसे अन्तःप्रेरणा भी कहा जा सकता है। यही है जीवधारी की वह मौलिक विशेषता, जिससे वह प्रगति पथ पर लाखों-करोड़ों वर्षों तक चलते-चलते इस स्थिति पर पहुंचा है जिसमें जीव जगत के अगणित प्राणियों को पाया जाता है। यह सृष्टि के आरंभ काल की तुलना में असंख्य गुना अधिक परिष्कृत है। आदिमकाल की अनगढ़ स्थिति और आज की स्थिति का कोई मुकाबला नहीं। उस समय के और आज के जीवधारियों की चेतना, कुशलता एवं क्षमता में आश्चर्यजनक अन्तर पाया जाता है। अनगढ़ जीवसत्ता ने आज की सुगढ़ स्थिति प्राप्त करने में असाधारण प्रयास-पुरुषार्थ का परिचय दिया है। इस प्रगति में प्रकृति एवं परिस्थितियों का योगदान न रहा हो ऐसी बात नहीं, किन्तु जिसे भौतिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं वह अन्तराल की वह उमंग ही है जो आगे बढ़ने की निरन्तर प्रेरणा देती और उसके लिए पुरुषार्थ की बेचैनी बनाये रखती है।
इस संदर्भ में दो प्रवाह सामने आते हैं—एक चेतना पक्ष का ऊंचा उठना, दूसरा काय वैभव का आगे बढ़ना। ऊंचा उठने से तात्पर्य है चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का अभिवर्धन। आगे बढ़ने का अर्थ है—समर्थता और सम्पदा का उपार्जन। इन दोनों के समन्वय से जीवन की दिशाधारा बनती है। मान्यता और आकांक्षा का स्तर श्रेष्ठ या निकृष्ट होना व्यक्ति का अपना चुनाव है, जो इसे वरण करेगा वह उस दिशा में अग्रसर अवश्य होगा। जिनकी गति धीमी होती है, उनकी आलसी-प्रमादी आदि नामों से भर्त्सना की जाती है। ऐसे ही लोग पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं और अभाव-उपहास के भाजन बनते हैं। जिनकी दिशाधारा सही होती है वे वैभव-सम्मान पाते और श्रेय-संतोष के अधिकारी बनते हैं। यह समस्त उपलब्धियां उस आकांक्षा तत्व की हैं जो न्यूनाधिक मात्रा में सभी में पायी जाती है।
प्रगति की आकांक्षा स्वाभाविक भी है और उचित उपयोगी भी। उसमें व्यक्ति का निजी लाभ भी है और समाज का समग्र हित-साधन भी। इच्छा के त्याग वाली उक्ति जिन अध्यात्म ग्रन्थों में पाई जाती है, वहां उनका प्रयोजन प्रतिफल का, आतुरता का परित्याग करने भर से है। शब्दावली में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनसे किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुरे कामों के परिणाम तो तत्काल भी मिल जाते हैं, पर भले कामों का उपयुक्त प्रतिफल मिलने में क्षमता और पुरुषार्थ के निर्धारण की एवं साधन की परिस्थितिजन्य अनुकूलता की कमी रहने पर अभीष्ट सत्परिणामों की मात्रा तथा अवधि में व्यतिरेक हो सकता है। ऐसी दशा में कर्त्ता को जो खीझ, निराशा एवं अनास्था उत्पन्न होती है, उसी की रोकथाम के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि सत्कर्म से मिलने वाले संतोष एवं सन्मार्ग पर चलने के गौरव को पर्याप्त प्रतिफल मान लिया जाय और समयानुसार जब भी सत्परिणाम उपलब्ध हो तब उसे अतिरिक्त उपहार भर माना जाय। इस मान्यता को अपनाने से संतुलन बना रहता है और मार्ग से विचलित होने में उद्विग्नताजन्य अवरोध बाधक नहीं बन पाता।
सृष्टि के आदि में सृष्टा ने इच्छा की कि ‘मैं एक से अनेक जाऊं और अपने अनेक रूपों के साथ रमण की क्रीड़ा-कल्लोल में निरत रहूं।’ यह इच्छा ही परा और अपरा के रूप में प्रादुर्भूत हुई और सृष्टिक्रम चल पड़ा। प्राणियों में यह इच्छा प्रगति की अभिलाषा के रूप में पाई जाती है और पदार्थों में गतिशील बने रहने का पराक्रम अनुशासन बनकर रहती है, यही सुनियोजित होने पर प्रगति कहलाती है। उद्भव परिष्कार और परिवर्तन का नियति चक्र इसी धुरी पर घूमता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इसी गोलाकार परिभ्रमण के नाम हैं। ब्रह्माण्ड के सभी छोटे-बड़े क्रिया-कलाप इसी दैवी निर्धारण अनुशासन के अन्तर्गत चल रहे हैं।
प्रगति के लिए प्रेरणा देने वाली आकांक्षा जीवसत्ता के साथ अनादिकाल से जुड़ी हुई है और अनन्तकाल तक जुड़ी रहेगी, उसे उपयुक्त दिशा देना ही मानवी बुद्धिमत्ता का चरम कौशल है—इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। आत्म निरीक्षण, आत्म निर्माण, आत्म सुधार, आत्म विकास के नाम से जिस आत्मोत्कर्ष एवं आत्म कल्याण का ऊहापोह होता रहता है, उसमें करने योग्य पराक्रम एक ही है कि आकांक्षाओं को, चेतना को सुसंस्कृत बनाने वाली उत्कृष्टता अपनाने के लिए बाधित किया जाय—इन मान्यताओं को ही श्रद्धा कहते हैं। यह आप्त कथन अक्षरशः सत्य है कि जीवात्मा का रूप श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही बन जाता है।
प्रकृति प्रदत्त आकांक्षायें शरीर पर छाई रहती हैं और भूख, प्रजनन, अस्तित्व रक्षा में तृष्णा, वासना, अहंता के विविध रूपों में प्रकट-परिलक्षित होती रहती हैं। यह सामान्य प्रवाह की बात हुई जिसे समस्त जीवधारी अपनाते और सृष्टि का गतिचक्र चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते हुए जीवन लीला समाप्त करते हैं। इससे आगे का पक्ष वह है जिसे आत्मा या चेतना को उच्चस्तरीय प्रगति की ओर ले चलने वाला निर्धारण कह सकते हैं। इसमें दैवी प्रवाह को अपनाना पड़ता है, आस्थाओं को आस्तिकता के साथ, बुद्धि को आध्यात्मिकता के साथ नियोजित करना पड़ता है। यही अध्यात्म दर्शन एवं साधना का सारभूत सिद्धांत है, आत्मा की चेतना की प्रगति इसी पर निर्भर है।
उपरोक्त कथन प्रतिपादन से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जीवसत्ता की मूलभूत प्रवृत्ति आकांक्षा के वर्तमान स्वरूप का पर्यवेक्षण किया जाय और देखा जाय कि वह शरीर को आगे बढ़ने और आत्मा की ऊंचे उठने की प्रवृत्ति को साथ-साथ लेकर चल रही है या नहीं। दोनों के बीच असंतुलन तो नहीं बन रहा है। असंतुलन से ही प्रगति, अवनति या दुर्गति होती है।
मनुष्य यदि सचमुच कह बुद्धिमान हो तो उसे समग्र प्रगति का दूरदर्शी निर्धारण करना चाहिए। यदि वह इतना कर सके तो समझना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान चेतना का वह अधिष्ठाता-अधिपति हो गया। उस सम्पदा का सही उपयोग जिसने भी किया है वह प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचा है और हर दृष्टि से कृत-कृत्य बना है। हमें प्रगति और अवनति के अन्तर को समझना चाहिए और अपनी वर्तमान परिस्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए औचित्य का विवेक सम्मत पर्यवेक्षण करना चाहिए। आत्मोत्कर्ष की परम श्रेयस्कर आकांक्षा को सुनियोजित करने में ही व्यक्ति का अभ्युदय और समाज का कल्याण है जो इतना समझने, स्वीकारने में समर्थ हो सकेगा उसका भविष्य सुनिश्चित रूप से उज्ज्वल बनकर रहेगा।
जीवन मुक्ति का वास्तविक आनन्द कैसे मिले :
आत्मा की आकांक्षाओं, मान्यताओं और भावनाओं को क्रियान्वित करने का भार मन को वहन करना पड़ता है। वही कार्यान्वयन की योजना बनाकर शरीर को देता है, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के सहारे वह उन्हें चरितार्थ करता रहता है। प्रत्यक्ष कृत्य शरीर करता है, इसलिए दोष अथवा श्रेय उसी को मिलता है, पर यह भुला दिया जाता है कि शरीर जड़ पंचतत्वों का बना हुआ है। उसमें न सोचने की क्षमता है और न करने की। रेल, मोटर-साइकिल आदि यंत्र वाहन अपनी मर्जी से भला-बुरा कुछ भी करने में असमर्थ हैं, ड्राइवर ही उन्हें जहां-तहां घसीटते फिरते हैं, यही विधा जीवनक्रम में चरितार्थ होती है।
आत्मा का परिधान अन्तःकरण है, उससे चेतना प्रभावित होती है। समर्थ एवं परिष्कृत आत्माएं साधना द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को उत्कृष्टता के ढांचे में ढाल लेती हैं। फलतः व्यक्तित्व परिष्कृत स्तर का बनता है और मनुष्य कलेवर में देवत्व की आभा झलकती है। इसके विपरीत यदि तमोगुणी असुरता अन्तराल की गहराई तक चली जाय तो प्रवृत्ति एवं आकांक्षा अनुपयुक्त कामों में रस लेती है और फिर तद्नुरूप प्रवृत्तियों का प्रवाह बहने लगता है।
आन्तरिक दुष्प्रवृत्तियों में वासना, तृष्णा और अहंता का असामान्य, उद्धत हो उठना अनेकानेक दोष-दुर्गुणों का सृजन करता है, यही प्रमुख मनोविकार हैं। क्रियाओं में यही उभरते दीखते हैं, किन्तु वस्तुतः उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त तीन दुष्प्रवृत्तियों का फलितार्थ ही उसे समझा जाना चाहिए। वासना और तृष्णाजन्य विकृतियों की चर्चा तो प्रायः की जाती है किन्तु मूलतः अहंता पर विचार किया जाना चाहिए, यह अहंकार का दूसरा नाम है। व्यक्ति अपने आप को दूसरों की निगाहों में वरिष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है और उसके लिए अनेक तरह के सरंजाम जुटाता है। यों इसका सीधा, सरल और सौम्य मार्ग है कि साधारण लोग गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से हेय जीवन जीते हैं, षट्-रिपुओं के चंगुल में बुरी तरह फंसे होते हैं। फलतः चिन्तन और चरित्र की दृष्टि से उनकी स्थिति नर-पशु, नर-पामर या नर-पिशाच जैसी होती है। इन दुष्प्रवृत्तियों के क्षेत्र में कौन अग्रणी रहा—इसी की प्रतिस्पर्धा उनमें चलती रहती है। इसी हेय स्तर की सफलताओं को अपनी चतुरता, कुशलता एवं सफलता के नाम से दिखाते-बखानते रहते हैं। औसत आदमी की अहंता इसी रूप में प्रकट होती है। दुष्ट-दुराचारी अपने अनीति कृत्यों को गौरव-गरिमा में सम्मिलित करते हैं और छल-प्रपंच की अनीति और आक्रमण की घटनाओं को अपनी विशिष्टता के रूप में देखते और दिखाते हैं।
यदि इस कुपंथ को उलटकर सज्जनोचित शालीनता अपनाई जा सके तो वह वास्तविक प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आधार बन जाती है। उतने भर से आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव और आत्मोत्कर्ष की स्थिति बन जाती है। लोगों का यह मिथ्या भ्रम है कि ओछे हथकण्डे अपनाकर येनकेन प्रकारेण अपनी महिमा का विज्ञापन किया जा सकता है। इस आधार पर प्रशंसा करने वाले दूसरे ही क्षण मुंह फेरने और निन्दा करने में भी नहीं चूकते। सामने वाले की चापलूसी परदा हटते ही यथार्थता बखानने लगती हैं। फैशन, सज-धज, अमीरों जैसे ठाट-बाट, किसी दुर्बल पर आक्रमण, किसी सज्जन को ठगना, घर में विपुल सम्पदा जमा करना, चाटुकारों का मुंह मीठा करके अपनी प्रशंसा सुनना आदि करतूतें उद्धत अहंता वाले लोग करते रहते हैं और उसी में अपन ढेरों समय, श्रम, धन तथा चिंतन गंवाते फिरते हैं। इस आधार पर जो प्रदर्शनात्मक प्रपंच खड़ा किया गया था वह क्षणिक और अवास्तविक विडम्बना खड़ा करने के अतिरिक्त और किसी अन्य काम नहीं आता।
शृंगारिक वेश-विन्यास बनाने वाले, कीमती वस्त्र-आभूषणों से लदने और तेल-फुलेल से महकने वाले लड़की-लड़के सोचते हैं कि वे जिस राह भी निकलेंगे उधर ही दर्शक उनकी कलाकारिता, सुन्दरता एवं सम्पन्नता को सराहेंगे, पर होता उससे ठीक उल्टा है। उनके चरित्र पर उंगली उठती है, दुराचार का आमंत्रण देते फिरने वाला माना जाता है। फिजूलखर्च को अदूरदर्शी एवं बाल-बुद्धि बचकाना माना जाता है, शृंगारिकता हर किसी पर यही छाप छोड़ती है, भले ही किसी अनुचित लाभ के लिए कोई मुंह सामने कुछ प्रशंसा के शब्द कह दे।
सादगी का सघन संबंध उच्च विचारों से है। गांधी, ईसा, बुद्ध जैसों के परिधान सस्ते और स्वल्प थे। ऋषि और महापुरुष भी अपनी सज्जा औसत देशवासियों से अधिक महंगी नहीं होने देते थे—यह शालीनता के परिधान हैं। इस प्रकार के आच्छादन से किसी की प्रतिष्ठा घटती नहीं वरन् बढ़ती है। महंगे वस्त्र और महंगे आभूषण पहनने, धारण किये फिरने वालों को स्वांग-नाटकों के प्रदर्शनकारी माना जाता है अथवा यह कहा जाता है कि पैसे को उपयुक्त कार्य में लगाकर सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाने की अपेक्षा मूर्खता द्वारा अपव्यय का कैसा कौतुक किया जा रहा है। अहंता का सबसे घटिया प्रदर्शन साज-सज्जा की शृंगारिकता के रूप में ही होता देखा जाता है।
समाज में फैली हुई बुराइयों में अपनी बुराइयों को बढ़-चढ़कर सिद्ध करने पर उस स्तर के लोग प्रशंसा करेंगे ही। जेल में बन्द अपराधियों में जो अपनी करतूतों का अधिक दिलचस्प और भयानक विवरण सुनाते हैं, उनकी बात सुनकर दूसरे लोग अवाक् तो रह जाते हैं, पर कभी अवसर पड़ने पर उनका साथ देने के लिए भूलकर भी तैयार नहीं होते। सोचते हैं कि ऐसे लोग किसी की भी हजामत बना सकते हैं। इनका कोई सगा-संबंधी नहीं होता, वे जिसके साथ मित्रता जोड़ते हैं पहले उसी को हलाल करते हैं। दुष्कर्मों में दिखाई गई धूर्तता या निष्ठुरता किसी के लिए गौरव या प्रतिष्ठा की बात नहीं हो सकती, ऐसे लोगों पर दसों दिशाओं से घृणा और भर्त्सना बरसती है। रण्डी-भडुए आपस में मीठी बाते करते हैं और आदान-प्रदान भी पर दोनों में से कोई किसी का मित्र नहीं होता। मौका पड़ने पर उन्हें मुंह मोड़ने में ही नहीं घात मारने में भी देर नहीं लगती। दुर्जनों का संसार भर में न कोई प्रशंसक होता है और न सहयोगी। सज्जनता अपनाने वालों की मुंह आगे प्रशंसा भले ही न हो, भीतर से हर व्यक्ति उनके लिए श्रद्धा रखता है और सहयोग की भावना भी। यह किसी प्रकार कम महत्व की उपलब्धियां नहीं है। महापुरुष सामान्य स्थिति से ऊंचा उठकर महान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, इससे सज्जनता के आधार पर उपलब्ध हुआ सम्मान और सहयोग ही प्रधान कारण होता है।
अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने, शेखी बघारने वाले को आत्मश्लाघाग्रस्त मनोरोगी माना जाता है। सज्जनों का सुनिश्चित गुण है—नम्रता और विनयशीलता, उनकी सादगी देखते ही बनती है। महामना मदनमोहन मालवीयजी को सरकार ने ‘सर’ की उपाधि दे रखी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद ‘डाक्ट्रेट’ स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। पंडित महासभा ने उन्हें पंडित शिरोमणि की उपाधि दी थी। इन तीनों पदवियों को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया और कहा—मेरे पिताजी ‘पंडित’ की परम्परागत उपाधि दे गये हैं उसका निर्वाह ही मुझे भारी प्रतीत होता है फिर और उपाधियों से लदकर उन्हें वहन कर सकना मेरे लिए कैसे संभव हो सकेगा। यह नम्रता एक का उदाहरण है, इस कारण मालवीयजी की गरिमा घटी नहीं वरन् बढ़ी है। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर जैसे संत अपना परिचय सामान्य लोगों की पंक्ति में खड़े होकर ही देते रहे हैं। यदि उनने बड़प्पन की प्रशंसात्मक डींगें हांकी होतीं तो निश्चित रूप से वे विज्ञजनों की दृष्टि में गये-गुजरे ही गिने गये होते।
मनुष्य के लिए यह क्या कम गौरव की बात है कि वह परमेश्वर का युवराज है। इस पदवी को सार्थक बनाने के लिए उसे अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व ऐसा बनाना चाहिए जो उस गरिमा के अनुरूप हो, इसके लिए अपनी निजी पवित्रता और प्रखरता उच्च स्तर की विनिर्मित करनी चाहिए। निजी अभिलाषाओं को इतना कम करना चाहिए कि उसे अपरिग्रही ब्राह्मण कहा जा सके। ब्राह्मण को भगवान भी अपेक्षाकृत अधिक प्यार करते हैं और चारों वर्णों में उसकी श्रेष्ठता मानी गयी है। इसका एक ही कारण है कि उसका निजी निर्वाह अत्यन्त साधारण होता है और अभिमान इतना गलित होता है कि भीख मांगने में भी अवमानना अनुभव न करे—यह नम्रता की चरम सीमा है—जिस तरह फलों से लदे हुए वृक्ष की हर डाली नीचे झुक जाती है।
आत्म गौरव की अनुभूति और लोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है—पुण्य-परोपकार में रसानुभूति और लोक सेवा में निरन्तर प्रवृत्ति। जो इस मार्ग को अपनाते हैं वे हर घड़ी अपनी और दूसरों की दृष्टि में गौरव-गरिमा से भरे-पूरे माने जाते हैं। इसके बिना अन्य पगडण्डियां खोजने वाले कांटों में उलझते और भटकाव में फंसते हैं। सूरज, चन्द्रमा निस्वार्थ भाव से प्रकाश वितरण के लिए निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं। बादलों के लिए एक ही काम है कि समुद्र से पानी लाना और सूखे भूखण्डों में शीतलता एवं हरीतिमा उगाना। वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं, पवन दूसरों के लिए चलता और अग्नि दूसरों के लिए जलती है—यह श्रेष्ठतम् कर्तृत्व ही उन्हें भरपूर सम्मान प्रदान करता है, इससे बढ़कर अहंता की पूर्ति और क्या हो सकती है। मनुष्य को भगवान के विश्व-उद्यान का माली बनाकर भेजा गया है और दायित्व सौंपा गया है कि वह उसे सुन्दर, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने में तत्परता और तन्मयता के साथ लगा रहे। यह लगन जिसकी जितनी बढ़ी-चढ़ी होगी उसकी अहंता उतनी ही विगलित होती जायेगी। इस आधार पर भारमुक्त हुई आत्मा इसी शरीर के रहते हुए जीवनमुक्त का आनन्द उपलब्ध करेगी।
देवमानव बनने का आह्वान :
नृतत्त्ववेत्ताओं ने विविध पर्यवेक्षणों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आदिमानव-वनमानुष स्तर का था। उसमें पशु प्रवृत्तियों का बाहुल्य था, रहन-सहन और क्रिया-कलाप भी उसी स्तर का था। प्रकृति के अनुदानों पर पशु-पक्षियों की तरह अपना जीवन निर्वाह करता था, प्रगति की दिशा में उसके कुछ चरण और आगे बढ़े तो पुरुषार्थ-परायण हुआ। कृषि, पशुपालन जैसे उद्योग सीखे, वस्त्र, निवास, अग्नि प्रज्ज्वलन जैसी विधि-व्यवस्थाओं से अवगत हो गया। बोलना-लिखना सीख गया और अपने-अपने समुदायों के प्रथा-प्रचलनों का अभ्यस्त हो गया। भौतिक प्रगति इसी दिशा में प्रगतिशील होती चली आई है। विज्ञान, यंत्रीकरण, अर्थशास्त्र, शासनतंत्र की उपलब्धियों के सहारे वह वहां पहुंचा है जहां आज है। उसके सामने सुविधा-साधनों का बाहुल्य है। यह दूसरी बात है कि अपने व्यक्तित्व को घटिया बनाये रहकर वह उसका सही-समुचित उपयोग न कर सके। मानवी प्रगति का यही लेखा-जोखा है। मनुष्यों में से कुछ उद्दण्ड, अत्याचारी, छली, आक्रामक, विलासी व अहंकारी बन गये हैं और कुछ को अपनी नासमझी और कुशलता-प्रतिभा के अभाव में गई-गुजरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। मनुष्य को बन्दर की औलाद इसलिए कहा जाता है कि उसकी भावना और विचारणा पेट-प्रजनन के इर्द-गिर्द घूमती है, पेट-प्रजनन के लिए वह मरता-खपता है। बहुत हुआ तो ठाट-बाट बनाना, दर्प जताना और आक्रामक बनकर अपनी विशिष्टता सिद्ध करता है। जो इतना नहीं कर पाते वे परिस्थितियों की प्रतिकूलता और भाग्य की विपरीतता को कोसते हुए दिन गुजारते हैं। मनुष्यों में से अधिकांश तो इन्हीं आदिमानव, वनमानुष या धूर्त-शृंगाल प्रकृति के देखे जाते हैं। जनसंख्या की विपुलता ने न तो लोगों को निज की गौरव-गरिमा प्रदान की है और न समाज को समुन्नत-सुसंस्कृत बनाने में ही योगदान दिया है। चकाचौंध उत्पन्न करने वाली विडम्बना तो चारों और बिखरी अवश्य दिखाई देती है, पर उसकी परिणति-प्रतिक्रियाओं को देखते हुए निराशा ही होती है और असमंजस होता है कि जिसे ईश्वर का युवराज, प्राणी वर्ग में शिरोमणि-देवमानव आदि के नामों से सम्मानित किया गया है, क्या वह यही है? जिसे लोभ, मोह, स्वार्थ, वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं।
प्रकृति परायणता की सीमा इतनी है। जीवधारी अपने लिए ही जीते हैं, अपनी ही आवश्यकता को जुटाते और अपनी ही प्रसन्नता-अनुकूलता संजोने में निरत रहते हैं। प्रकृति परायण होकर भी मनुष्य उसी गई गुजरी स्थिति में रह सकता है जिसमें कि अन्य जीवधारी मरते और मारते हैं, गिरते और गिराते हैं।
मानवी गरिमा का उज्ज्वल स्वरूप विकसित प्रस्फुटित तब होता है जब वह उत्कृष्ट आदर्शवादिता के साथ अपना संबंध जोड़ता है। अपने चिन्तन, चरित्र व्यवहार और प्रयास को अभिनन्दनीय-अनुकरणीय बनाता है। इसी ढांचे में उसे ढालने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की है, अध्यात्म दर्शन का ढांचा खड़ा किया है। योग-तप के अनेक विधान बनाये हैं, ईश्वर भक्ति के अनेकानेक उपचार-कर्मकाण्डों का सृजन किया है। इन आत्मोत्कर्ष की अनेकानेक विधि-व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य इसी जीवन में स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि प्राप्त करे। यह तीनों ही किसी अन्य लोक से संबंधित या जादू-चमत्कार जैसी नहीं है वरन् उन्हें व्यक्तिगत महानता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दृष्टिकोण का परिष्कार ही ‘स्वर्ग’ है, दुष्प्रवृत्तियों से छूट निकलना ‘मुक्ति’ और अभिनन्दनीय स्तर पर जीवनचर्या को बनाये रखना ‘सिद्धि’। आत्मोत्कर्ष के लिए इतना करना ही पर्याप्त है। इससे कम में उस प्रयोजन की पूर्ति होती नहीं, इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों, सिद्ध पुरुषों, महामानवों को इसी आत्मिक प्रगति-प्रयास में संलग्न पाया गया है। उनने आकाशवासी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया वह वस्तुतः अपने ही भीतर के देवता को जगाने के लिए किया था।
मनुष्य को सुनिश्चित रूप से अपने भाग्य का निर्माता कहा गया है, वह इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करता है। अपने आप को अधिकाधिक पवित्र, परिष्कृत, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान् बनाता है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर लेता है। अन्तःकरण और बाह्याचरण में जब समान रूप से उत्कृष्टता का समावेश हो तो सामान्य शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति देवमानव की गरिमा उपलब्ध कर लेता है। ऐसे लोगों के लिए देवमानव नाम दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। देवता अशरीरी होते हैं, इसलिए उनके साथ प्रत्यक्ष घुलना-मिलना नहीं हो सकता, पर देवमानवों को संत, सुधारक और शहीदों के रूप में प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। ऐसे नर देवपुरुष-पुरुषोत्तम होते तो कम ही है, पर उनका सर्वथा अभाव किसी भी युग में नहीं होता। सतयुग में ऐसे ही लोगों का बाहुल्य था। भारतभूमि के तैंतीस कोटि निवासी संसार भर में तैंतीस कोटि देवताओं के नाम से प्रख्यात हैं। जिस धरती पर वे जन्मते-पलते थे वह ‘स्वर्गादपि गरीयसी’ कही जाती थी। उनके अच्छे क्रिया-कलापों से वातावरण इतना दिव्य बन जाता था कि उसे सतयुग नाम दिया जाना उपयुक्त ही जंचता था, यह समय लम्बी अवधि तक बना रहा। इनके शरीर भी प्रकृति प्रदत्त थे, पर उनके अन्तःकरण में देवत्व कूट-कूटकर भरा था। डिब्बी के भीतर जो वस्तु रखी है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। जिनकी अन्तरात्मा प्रामाणिकता, शालीनता, सेवा और पुरुषार्थ परायणता से सराबोर है उन्हें देवतुल्य ही नहीं वरन् उससे बढ़कर माना जा सकता है। देवता अप्रत्यक्ष होते हैं, मनुहार करने और उपहार देने पर पसीजते हैं। इसके उपरान्त ही उनके वरदान-अनुदान साधकों पर बरसते हैं किन्तु देवमानवों की कृपा-अनुकम्पा अहैतुकी होती है और बिना याचना की प्रतीक्षा किये मेघमाला की तरह बरसती और बसन्त की तरह शोभा-सुषमा से सर्वत्र उल्लास बिखेरती है।
भारत देवभूमि है। स्वर्गलोक के अस्तित्व को चुनौती दिये बिना कहा जा सकता है कि यदि उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो ऐसे महामानवों की उपस्थिति अभी भी जहां-तहां देखी जा सकती है। सतयुग में तो वे साधु-ब्राह्मण के रूप में एक विकसित समुदाय के रूप में ही इस धरित्री की शोभा, सुषमा, संस्कृति एवं समृद्धि का सम्वर्धन करते थे। आज मनुष्य की व्यक्तिगत सामूहिक समस्यायें बेतरह उलझ गई हों, साधन-सामग्री घट गई हों सो बात नहीं है। विज्ञान और कौशल ने साधनों का अतिशय विस्तार किया है, किन्तु व्यक्तित्व की दृष्टि से समुदाय अतिशय बौना हो गया है। कुछ उत्पीड़क हैं, कुछ उत्पीड़ित। कुछ शोषक हैं, कुछ शोषित। कुछ पर्वत की चोटी पर बैठे हैं तो कुछ खाई में गिरकर कराह रहे हैं। इस विषमता को समता में परिणत करने के लिए देवमानवों के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं हो सकता।
पौराणिक कथानकों में अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन के निमित्त अवतारों का प्रकटीकरण होता रहा है। इस अलंकारिक प्रतिपादन का व्यावहारिक स्वरूप यह हो सकता है कि प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता की पक्षधर उदारता सामान्य लोगों जैसी गतिविधियों से उबारकर देव प्रयोजनों में जुट जाने का एकाकी प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सद्भावनापूर्वक अपनाये गये उच्च स्तरीय निर्धारणों को पूरा करने में कर्त्ता की अन्तरात्मा और दैवी शक्तियों की अनुकम्पा समान रूप से, संयुक्त रूप से काम करती है और जो परिणाम सामने आते हैं वे चमत्कारी स्तर के होते हैं। परमार्थी पुरोहितों को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। वस्तुतः वे ही समाज का स्तर, परिस्थितियों का प्रवाह और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते और सफल होकर रहते हैं। समय की पुकार है कि ऐसे उदारचेता उभरें, अपने इर्द-गिर्द के भव-बन्धनों की पकड़ से अपने को उबारें और साथ ही जन-कल्याण की उन प्रवृत्तियों में जुटें जिन्हें प्रकारान्तर से अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापन भी कहा जा सकता है। परिस्थितियों की मांग इतनी प्रबल है कि इससे बच निकलने के लिए कोई बहाना नहीं खोजा जाना चाहिए। सतयुग का माहौल बनाने के लिए भावनाशीलों को संकल्पपूर्वक आगे आना चाहिए, आज की परिस्थितियों में रीति-नीति के अपनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। साधु और ब्राह्मणों को भूसुर-पृथ्वी के देवता कहा जाता है, वे अपनी योग्यता, श्रमशीलता, सम्पदा का न्यूनतम अंश अपने निर्वाह के लिए रखते हैं और शेष को अन्यान्यों को उठाने-बढ़ाने में खर्च करने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। किसी के निवेदन की प्रतीक्षा नहीं करते, बादलों की तरह बिना बुलाये ही सर्वत्र पहुंचते हैं और हर किसी को समुन्नत-सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयास करते हैं—ऐसे ही देवमानवों की संख्या बढ़ने से धरती का वातावरण स्वर्गोपम बनता है।
प्रकृति ने जीवधारियों के निर्वाह की सुविधा स्वेच्छापूर्वक प्रदान की है। ऐसा न होता तो जीवन के लिए अपना अस्तित्व बनाये रहना, अपनी प्रगति के साधन-सामग्री उपलब्ध कर सकना ही संभव न होता, तब उन्नति करने और समग्र-समर्थ होने की बात ही कैसे बनती? इतने पर भी यह मानकर चलना होगा कि जीवधारी का अपना निजी स्वभाव अग्रगमन के लिए, अभ्युदय के लिए अनवरत पुरुषार्थ करना है। इसी को इच्छा, अभिलाषा और आकांक्षा कहते हैं, इसे अन्तःप्रेरणा भी कहा जा सकता है। यही है जीवधारी की वह मौलिक विशेषता, जिससे वह प्रगति पथ पर लाखों-करोड़ों वर्षों तक चलते-चलते इस स्थिति पर पहुंचा है जिसमें जीव जगत के अगणित प्राणियों को पाया जाता है। यह सृष्टि के आरंभ काल की तुलना में असंख्य गुना अधिक परिष्कृत है। आदिमकाल की अनगढ़ स्थिति और आज की स्थिति का कोई मुकाबला नहीं। उस समय के और आज के जीवधारियों की चेतना, कुशलता एवं क्षमता में आश्चर्यजनक अन्तर पाया जाता है। अनगढ़ जीवसत्ता ने आज की सुगढ़ स्थिति प्राप्त करने में असाधारण प्रयास-पुरुषार्थ का परिचय दिया है। इस प्रगति में प्रकृति एवं परिस्थितियों का योगदान न रहा हो ऐसी बात नहीं, किन्तु जिसे भौतिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं वह अन्तराल की वह उमंग ही है जो आगे बढ़ने की निरन्तर प्रेरणा देती और उसके लिए पुरुषार्थ की बेचैनी बनाये रखती है।
इस संदर्भ में दो प्रवाह सामने आते हैं—एक चेतना पक्ष का ऊंचा उठना, दूसरा काय वैभव का आगे बढ़ना। ऊंचा उठने से तात्पर्य है चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का अभिवर्धन। आगे बढ़ने का अर्थ है—समर्थता और सम्पदा का उपार्जन। इन दोनों के समन्वय से जीवन की दिशाधारा बनती है। मान्यता और आकांक्षा का स्तर श्रेष्ठ या निकृष्ट होना व्यक्ति का अपना चुनाव है, जो इसे वरण करेगा वह उस दिशा में अग्रसर अवश्य होगा। जिनकी गति धीमी होती है, उनकी आलसी-प्रमादी आदि नामों से भर्त्सना की जाती है। ऐसे ही लोग पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं और अभाव-उपहास के भाजन बनते हैं। जिनकी दिशाधारा सही होती है वे वैभव-सम्मान पाते और श्रेय-संतोष के अधिकारी बनते हैं। यह समस्त उपलब्धियां उस आकांक्षा तत्व की हैं जो न्यूनाधिक मात्रा में सभी में पायी जाती है।
प्रगति की आकांक्षा स्वाभाविक भी है और उचित उपयोगी भी। उसमें व्यक्ति का निजी लाभ भी है और समाज का समग्र हित-साधन भी। इच्छा के त्याग वाली उक्ति जिन अध्यात्म ग्रन्थों में पाई जाती है, वहां उनका प्रयोजन प्रतिफल का, आतुरता का परित्याग करने भर से है। शब्दावली में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनसे किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुरे कामों के परिणाम तो तत्काल भी मिल जाते हैं, पर भले कामों का उपयुक्त प्रतिफल मिलने में क्षमता और पुरुषार्थ के निर्धारण की एवं साधन की परिस्थितिजन्य अनुकूलता की कमी रहने पर अभीष्ट सत्परिणामों की मात्रा तथा अवधि में व्यतिरेक हो सकता है। ऐसी दशा में कर्त्ता को जो खीझ, निराशा एवं अनास्था उत्पन्न होती है, उसी की रोकथाम के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि सत्कर्म से मिलने वाले संतोष एवं सन्मार्ग पर चलने के गौरव को पर्याप्त प्रतिफल मान लिया जाय और समयानुसार जब भी सत्परिणाम उपलब्ध हो तब उसे अतिरिक्त उपहार भर माना जाय। इस मान्यता को अपनाने से संतुलन बना रहता है और मार्ग से विचलित होने में उद्विग्नताजन्य अवरोध बाधक नहीं बन पाता।
सृष्टि के आदि में सृष्टा ने इच्छा की कि ‘मैं एक से अनेक जाऊं और अपने अनेक रूपों के साथ रमण की क्रीड़ा-कल्लोल में निरत रहूं।’ यह इच्छा ही परा और अपरा के रूप में प्रादुर्भूत हुई और सृष्टिक्रम चल पड़ा। प्राणियों में यह इच्छा प्रगति की अभिलाषा के रूप में पाई जाती है और पदार्थों में गतिशील बने रहने का पराक्रम अनुशासन बनकर रहती है, यही सुनियोजित होने पर प्रगति कहलाती है। उद्भव परिष्कार और परिवर्तन का नियति चक्र इसी धुरी पर घूमता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इसी गोलाकार परिभ्रमण के नाम हैं। ब्रह्माण्ड के सभी छोटे-बड़े क्रिया-कलाप इसी दैवी निर्धारण अनुशासन के अन्तर्गत चल रहे हैं।
प्रगति के लिए प्रेरणा देने वाली आकांक्षा जीवसत्ता के साथ अनादिकाल से जुड़ी हुई है और अनन्तकाल तक जुड़ी रहेगी, उसे उपयुक्त दिशा देना ही मानवी बुद्धिमत्ता का चरम कौशल है—इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। आत्म निरीक्षण, आत्म निर्माण, आत्म सुधार, आत्म विकास के नाम से जिस आत्मोत्कर्ष एवं आत्म कल्याण का ऊहापोह होता रहता है, उसमें करने योग्य पराक्रम एक ही है कि आकांक्षाओं को, चेतना को सुसंस्कृत बनाने वाली उत्कृष्टता अपनाने के लिए बाधित किया जाय—इन मान्यताओं को ही श्रद्धा कहते हैं। यह आप्त कथन अक्षरशः सत्य है कि जीवात्मा का रूप श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही बन जाता है।
प्रकृति प्रदत्त आकांक्षायें शरीर पर छाई रहती हैं और भूख, प्रजनन, अस्तित्व रक्षा में तृष्णा, वासना, अहंता के विविध रूपों में प्रकट-परिलक्षित होती रहती हैं। यह सामान्य प्रवाह की बात हुई जिसे समस्त जीवधारी अपनाते और सृष्टि का गतिचक्र चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते हुए जीवन लीला समाप्त करते हैं। इससे आगे का पक्ष वह है जिसे आत्मा या चेतना को उच्चस्तरीय प्रगति की ओर ले चलने वाला निर्धारण कह सकते हैं। इसमें दैवी प्रवाह को अपनाना पड़ता है, आस्थाओं को आस्तिकता के साथ, बुद्धि को आध्यात्मिकता के साथ नियोजित करना पड़ता है। यही अध्यात्म दर्शन एवं साधना का सारभूत सिद्धांत है, आत्मा की चेतना की प्रगति इसी पर निर्भर है।
उपरोक्त कथन प्रतिपादन से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जीवसत्ता की मूलभूत प्रवृत्ति आकांक्षा के वर्तमान स्वरूप का पर्यवेक्षण किया जाय और देखा जाय कि वह शरीर को आगे बढ़ने और आत्मा की ऊंचे उठने की प्रवृत्ति को साथ-साथ लेकर चल रही है या नहीं। दोनों के बीच असंतुलन तो नहीं बन रहा है। असंतुलन से ही प्रगति, अवनति या दुर्गति होती है।
मनुष्य यदि सचमुच कह बुद्धिमान हो तो उसे समग्र प्रगति का दूरदर्शी निर्धारण करना चाहिए। यदि वह इतना कर सके तो समझना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान चेतना का वह अधिष्ठाता-अधिपति हो गया। उस सम्पदा का सही उपयोग जिसने भी किया है वह प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचा है और हर दृष्टि से कृत-कृत्य बना है। हमें प्रगति और अवनति के अन्तर को समझना चाहिए और अपनी वर्तमान परिस्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए औचित्य का विवेक सम्मत पर्यवेक्षण करना चाहिए। आत्मोत्कर्ष की परम श्रेयस्कर आकांक्षा को सुनियोजित करने में ही व्यक्ति का अभ्युदय और समाज का कल्याण है जो इतना समझने, स्वीकारने में समर्थ हो सकेगा उसका भविष्य सुनिश्चित रूप से उज्ज्वल बनकर रहेगा।
जीवन मुक्ति का वास्तविक आनन्द कैसे मिले :
आत्मा की आकांक्षाओं, मान्यताओं और भावनाओं को क्रियान्वित करने का भार मन को वहन करना पड़ता है। वही कार्यान्वयन की योजना बनाकर शरीर को देता है, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के सहारे वह उन्हें चरितार्थ करता रहता है। प्रत्यक्ष कृत्य शरीर करता है, इसलिए दोष अथवा श्रेय उसी को मिलता है, पर यह भुला दिया जाता है कि शरीर जड़ पंचतत्वों का बना हुआ है। उसमें न सोचने की क्षमता है और न करने की। रेल, मोटर-साइकिल आदि यंत्र वाहन अपनी मर्जी से भला-बुरा कुछ भी करने में असमर्थ हैं, ड्राइवर ही उन्हें जहां-तहां घसीटते फिरते हैं, यही विधा जीवनक्रम में चरितार्थ होती है।
आत्मा का परिधान अन्तःकरण है, उससे चेतना प्रभावित होती है। समर्थ एवं परिष्कृत आत्माएं साधना द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को उत्कृष्टता के ढांचे में ढाल लेती हैं। फलतः व्यक्तित्व परिष्कृत स्तर का बनता है और मनुष्य कलेवर में देवत्व की आभा झलकती है। इसके विपरीत यदि तमोगुणी असुरता अन्तराल की गहराई तक चली जाय तो प्रवृत्ति एवं आकांक्षा अनुपयुक्त कामों में रस लेती है और फिर तद्नुरूप प्रवृत्तियों का प्रवाह बहने लगता है।
आन्तरिक दुष्प्रवृत्तियों में वासना, तृष्णा और अहंता का असामान्य, उद्धत हो उठना अनेकानेक दोष-दुर्गुणों का सृजन करता है, यही प्रमुख मनोविकार हैं। क्रियाओं में यही उभरते दीखते हैं, किन्तु वस्तुतः उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त तीन दुष्प्रवृत्तियों का फलितार्थ ही उसे समझा जाना चाहिए। वासना और तृष्णाजन्य विकृतियों की चर्चा तो प्रायः की जाती है किन्तु मूलतः अहंता पर विचार किया जाना चाहिए, यह अहंकार का दूसरा नाम है। व्यक्ति अपने आप को दूसरों की निगाहों में वरिष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है और उसके लिए अनेक तरह के सरंजाम जुटाता है। यों इसका सीधा, सरल और सौम्य मार्ग है कि साधारण लोग गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से हेय जीवन जीते हैं, षट्-रिपुओं के चंगुल में बुरी तरह फंसे होते हैं। फलतः चिन्तन और चरित्र की दृष्टि से उनकी स्थिति नर-पशु, नर-पामर या नर-पिशाच जैसी होती है। इन दुष्प्रवृत्तियों के क्षेत्र में कौन अग्रणी रहा—इसी की प्रतिस्पर्धा उनमें चलती रहती है। इसी हेय स्तर की सफलताओं को अपनी चतुरता, कुशलता एवं सफलता के नाम से दिखाते-बखानते रहते हैं। औसत आदमी की अहंता इसी रूप में प्रकट होती है। दुष्ट-दुराचारी अपने अनीति कृत्यों को गौरव-गरिमा में सम्मिलित करते हैं और छल-प्रपंच की अनीति और आक्रमण की घटनाओं को अपनी विशिष्टता के रूप में देखते और दिखाते हैं।
यदि इस कुपंथ को उलटकर सज्जनोचित शालीनता अपनाई जा सके तो वह वास्तविक प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आधार बन जाती है। उतने भर से आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव और आत्मोत्कर्ष की स्थिति बन जाती है। लोगों का यह मिथ्या भ्रम है कि ओछे हथकण्डे अपनाकर येनकेन प्रकारेण अपनी महिमा का विज्ञापन किया जा सकता है। इस आधार पर प्रशंसा करने वाले दूसरे ही क्षण मुंह फेरने और निन्दा करने में भी नहीं चूकते। सामने वाले की चापलूसी परदा हटते ही यथार्थता बखानने लगती हैं। फैशन, सज-धज, अमीरों जैसे ठाट-बाट, किसी दुर्बल पर आक्रमण, किसी सज्जन को ठगना, घर में विपुल सम्पदा जमा करना, चाटुकारों का मुंह मीठा करके अपनी प्रशंसा सुनना आदि करतूतें उद्धत अहंता वाले लोग करते रहते हैं और उसी में अपन ढेरों समय, श्रम, धन तथा चिंतन गंवाते फिरते हैं। इस आधार पर जो प्रदर्शनात्मक प्रपंच खड़ा किया गया था वह क्षणिक और अवास्तविक विडम्बना खड़ा करने के अतिरिक्त और किसी अन्य काम नहीं आता।
शृंगारिक वेश-विन्यास बनाने वाले, कीमती वस्त्र-आभूषणों से लदने और तेल-फुलेल से महकने वाले लड़की-लड़के सोचते हैं कि वे जिस राह भी निकलेंगे उधर ही दर्शक उनकी कलाकारिता, सुन्दरता एवं सम्पन्नता को सराहेंगे, पर होता उससे ठीक उल्टा है। उनके चरित्र पर उंगली उठती है, दुराचार का आमंत्रण देते फिरने वाला माना जाता है। फिजूलखर्च को अदूरदर्शी एवं बाल-बुद्धि बचकाना माना जाता है, शृंगारिकता हर किसी पर यही छाप छोड़ती है, भले ही किसी अनुचित लाभ के लिए कोई मुंह सामने कुछ प्रशंसा के शब्द कह दे।
सादगी का सघन संबंध उच्च विचारों से है। गांधी, ईसा, बुद्ध जैसों के परिधान सस्ते और स्वल्प थे। ऋषि और महापुरुष भी अपनी सज्जा औसत देशवासियों से अधिक महंगी नहीं होने देते थे—यह शालीनता के परिधान हैं। इस प्रकार के आच्छादन से किसी की प्रतिष्ठा घटती नहीं वरन् बढ़ती है। महंगे वस्त्र और महंगे आभूषण पहनने, धारण किये फिरने वालों को स्वांग-नाटकों के प्रदर्शनकारी माना जाता है अथवा यह कहा जाता है कि पैसे को उपयुक्त कार्य में लगाकर सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाने की अपेक्षा मूर्खता द्वारा अपव्यय का कैसा कौतुक किया जा रहा है। अहंता का सबसे घटिया प्रदर्शन साज-सज्जा की शृंगारिकता के रूप में ही होता देखा जाता है।
समाज में फैली हुई बुराइयों में अपनी बुराइयों को बढ़-चढ़कर सिद्ध करने पर उस स्तर के लोग प्रशंसा करेंगे ही। जेल में बन्द अपराधियों में जो अपनी करतूतों का अधिक दिलचस्प और भयानक विवरण सुनाते हैं, उनकी बात सुनकर दूसरे लोग अवाक् तो रह जाते हैं, पर कभी अवसर पड़ने पर उनका साथ देने के लिए भूलकर भी तैयार नहीं होते। सोचते हैं कि ऐसे लोग किसी की भी हजामत बना सकते हैं। इनका कोई सगा-संबंधी नहीं होता, वे जिसके साथ मित्रता जोड़ते हैं पहले उसी को हलाल करते हैं। दुष्कर्मों में दिखाई गई धूर्तता या निष्ठुरता किसी के लिए गौरव या प्रतिष्ठा की बात नहीं हो सकती, ऐसे लोगों पर दसों दिशाओं से घृणा और भर्त्सना बरसती है। रण्डी-भडुए आपस में मीठी बाते करते हैं और आदान-प्रदान भी पर दोनों में से कोई किसी का मित्र नहीं होता। मौका पड़ने पर उन्हें मुंह मोड़ने में ही नहीं घात मारने में भी देर नहीं लगती। दुर्जनों का संसार भर में न कोई प्रशंसक होता है और न सहयोगी। सज्जनता अपनाने वालों की मुंह आगे प्रशंसा भले ही न हो, भीतर से हर व्यक्ति उनके लिए श्रद्धा रखता है और सहयोग की भावना भी। यह किसी प्रकार कम महत्व की उपलब्धियां नहीं है। महापुरुष सामान्य स्थिति से ऊंचा उठकर महान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, इससे सज्जनता के आधार पर उपलब्ध हुआ सम्मान और सहयोग ही प्रधान कारण होता है।
अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने, शेखी बघारने वाले को आत्मश्लाघाग्रस्त मनोरोगी माना जाता है। सज्जनों का सुनिश्चित गुण है—नम्रता और विनयशीलता, उनकी सादगी देखते ही बनती है। महामना मदनमोहन मालवीयजी को सरकार ने ‘सर’ की उपाधि दे रखी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद ‘डाक्ट्रेट’ स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। पंडित महासभा ने उन्हें पंडित शिरोमणि की उपाधि दी थी। इन तीनों पदवियों को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया और कहा—मेरे पिताजी ‘पंडित’ की परम्परागत उपाधि दे गये हैं उसका निर्वाह ही मुझे भारी प्रतीत होता है फिर और उपाधियों से लदकर उन्हें वहन कर सकना मेरे लिए कैसे संभव हो सकेगा। यह नम्रता एक का उदाहरण है, इस कारण मालवीयजी की गरिमा घटी नहीं वरन् बढ़ी है। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर जैसे संत अपना परिचय सामान्य लोगों की पंक्ति में खड़े होकर ही देते रहे हैं। यदि उनने बड़प्पन की प्रशंसात्मक डींगें हांकी होतीं तो निश्चित रूप से वे विज्ञजनों की दृष्टि में गये-गुजरे ही गिने गये होते।
मनुष्य के लिए यह क्या कम गौरव की बात है कि वह परमेश्वर का युवराज है। इस पदवी को सार्थक बनाने के लिए उसे अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व ऐसा बनाना चाहिए जो उस गरिमा के अनुरूप हो, इसके लिए अपनी निजी पवित्रता और प्रखरता उच्च स्तर की विनिर्मित करनी चाहिए। निजी अभिलाषाओं को इतना कम करना चाहिए कि उसे अपरिग्रही ब्राह्मण कहा जा सके। ब्राह्मण को भगवान भी अपेक्षाकृत अधिक प्यार करते हैं और चारों वर्णों में उसकी श्रेष्ठता मानी गयी है। इसका एक ही कारण है कि उसका निजी निर्वाह अत्यन्त साधारण होता है और अभिमान इतना गलित होता है कि भीख मांगने में भी अवमानना अनुभव न करे—यह नम्रता की चरम सीमा है—जिस तरह फलों से लदे हुए वृक्ष की हर डाली नीचे झुक जाती है।
आत्म गौरव की अनुभूति और लोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है—पुण्य-परोपकार में रसानुभूति और लोक सेवा में निरन्तर प्रवृत्ति। जो इस मार्ग को अपनाते हैं वे हर घड़ी अपनी और दूसरों की दृष्टि में गौरव-गरिमा से भरे-पूरे माने जाते हैं। इसके बिना अन्य पगडण्डियां खोजने वाले कांटों में उलझते और भटकाव में फंसते हैं। सूरज, चन्द्रमा निस्वार्थ भाव से प्रकाश वितरण के लिए निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं। बादलों के लिए एक ही काम है कि समुद्र से पानी लाना और सूखे भूखण्डों में शीतलता एवं हरीतिमा उगाना। वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं, पवन दूसरों के लिए चलता और अग्नि दूसरों के लिए जलती है—यह श्रेष्ठतम् कर्तृत्व ही उन्हें भरपूर सम्मान प्रदान करता है, इससे बढ़कर अहंता की पूर्ति और क्या हो सकती है। मनुष्य को भगवान के विश्व-उद्यान का माली बनाकर भेजा गया है और दायित्व सौंपा गया है कि वह उसे सुन्दर, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने में तत्परता और तन्मयता के साथ लगा रहे। यह लगन जिसकी जितनी बढ़ी-चढ़ी होगी उसकी अहंता उतनी ही विगलित होती जायेगी। इस आधार पर भारमुक्त हुई आत्मा इसी शरीर के रहते हुए जीवनमुक्त का आनन्द उपलब्ध करेगी।
देवमानव बनने का आह्वान :
नृतत्त्ववेत्ताओं ने विविध पर्यवेक्षणों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आदिमानव-वनमानुष स्तर का था। उसमें पशु प्रवृत्तियों का बाहुल्य था, रहन-सहन और क्रिया-कलाप भी उसी स्तर का था। प्रकृति के अनुदानों पर पशु-पक्षियों की तरह अपना जीवन निर्वाह करता था, प्रगति की दिशा में उसके कुछ चरण और आगे बढ़े तो पुरुषार्थ-परायण हुआ। कृषि, पशुपालन जैसे उद्योग सीखे, वस्त्र, निवास, अग्नि प्रज्ज्वलन जैसी विधि-व्यवस्थाओं से अवगत हो गया। बोलना-लिखना सीख गया और अपने-अपने समुदायों के प्रथा-प्रचलनों का अभ्यस्त हो गया। भौतिक प्रगति इसी दिशा में प्रगतिशील होती चली आई है। विज्ञान, यंत्रीकरण, अर्थशास्त्र, शासनतंत्र की उपलब्धियों के सहारे वह वहां पहुंचा है जहां आज है। उसके सामने सुविधा-साधनों का बाहुल्य है। यह दूसरी बात है कि अपने व्यक्तित्व को घटिया बनाये रहकर वह उसका सही-समुचित उपयोग न कर सके। मानवी प्रगति का यही लेखा-जोखा है। मनुष्यों में से कुछ उद्दण्ड, अत्याचारी, छली, आक्रामक, विलासी व अहंकारी बन गये हैं और कुछ को अपनी नासमझी और कुशलता-प्रतिभा के अभाव में गई-गुजरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। मनुष्य को बन्दर की औलाद इसलिए कहा जाता है कि उसकी भावना और विचारणा पेट-प्रजनन के इर्द-गिर्द घूमती है, पेट-प्रजनन के लिए वह मरता-खपता है। बहुत हुआ तो ठाट-बाट बनाना, दर्प जताना और आक्रामक बनकर अपनी विशिष्टता सिद्ध करता है। जो इतना नहीं कर पाते वे परिस्थितियों की प्रतिकूलता और भाग्य की विपरीतता को कोसते हुए दिन गुजारते हैं। मनुष्यों में से अधिकांश तो इन्हीं आदिमानव, वनमानुष या धूर्त-शृंगाल प्रकृति के देखे जाते हैं। जनसंख्या की विपुलता ने न तो लोगों को निज की गौरव-गरिमा प्रदान की है और न समाज को समुन्नत-सुसंस्कृत बनाने में ही योगदान दिया है। चकाचौंध उत्पन्न करने वाली विडम्बना तो चारों और बिखरी अवश्य दिखाई देती है, पर उसकी परिणति-प्रतिक्रियाओं को देखते हुए निराशा ही होती है और असमंजस होता है कि जिसे ईश्वर का युवराज, प्राणी वर्ग में शिरोमणि-देवमानव आदि के नामों से सम्मानित किया गया है, क्या वह यही है? जिसे लोभ, मोह, स्वार्थ, वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं।
प्रकृति परायणता की सीमा इतनी है। जीवधारी अपने लिए ही जीते हैं, अपनी ही आवश्यकता को जुटाते और अपनी ही प्रसन्नता-अनुकूलता संजोने में निरत रहते हैं। प्रकृति परायण होकर भी मनुष्य उसी गई गुजरी स्थिति में रह सकता है जिसमें कि अन्य जीवधारी मरते और मारते हैं, गिरते और गिराते हैं।
मानवी गरिमा का उज्ज्वल स्वरूप विकसित प्रस्फुटित तब होता है जब वह उत्कृष्ट आदर्शवादिता के साथ अपना संबंध जोड़ता है। अपने चिन्तन, चरित्र व्यवहार और प्रयास को अभिनन्दनीय-अनुकरणीय बनाता है। इसी ढांचे में उसे ढालने के लिए ऋषियों ने शास्त्रों की रचना की है, अध्यात्म दर्शन का ढांचा खड़ा किया है। योग-तप के अनेक विधान बनाये हैं, ईश्वर भक्ति के अनेकानेक उपचार-कर्मकाण्डों का सृजन किया है। इन आत्मोत्कर्ष की अनेकानेक विधि-व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य इसी जीवन में स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि प्राप्त करे। यह तीनों ही किसी अन्य लोक से संबंधित या जादू-चमत्कार जैसी नहीं है वरन् उन्हें व्यक्तिगत महानता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दृष्टिकोण का परिष्कार ही ‘स्वर्ग’ है, दुष्प्रवृत्तियों से छूट निकलना ‘मुक्ति’ और अभिनन्दनीय स्तर पर जीवनचर्या को बनाये रखना ‘सिद्धि’। आत्मोत्कर्ष के लिए इतना करना ही पर्याप्त है। इससे कम में उस प्रयोजन की पूर्ति होती नहीं, इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों, सिद्ध पुरुषों, महामानवों को इसी आत्मिक प्रगति-प्रयास में संलग्न पाया गया है। उनने आकाशवासी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया वह वस्तुतः अपने ही भीतर के देवता को जगाने के लिए किया था।
मनुष्य को सुनिश्चित रूप से अपने भाग्य का निर्माता कहा गया है, वह इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करता है। अपने आप को अधिकाधिक पवित्र, परिष्कृत, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान् बनाता है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर लेता है। अन्तःकरण और बाह्याचरण में जब समान रूप से उत्कृष्टता का समावेश हो तो सामान्य शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति देवमानव की गरिमा उपलब्ध कर लेता है। ऐसे लोगों के लिए देवमानव नाम दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। देवता अशरीरी होते हैं, इसलिए उनके साथ प्रत्यक्ष घुलना-मिलना नहीं हो सकता, पर देवमानवों को संत, सुधारक और शहीदों के रूप में प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। ऐसे नर देवपुरुष-पुरुषोत्तम होते तो कम ही है, पर उनका सर्वथा अभाव किसी भी युग में नहीं होता। सतयुग में ऐसे ही लोगों का बाहुल्य था। भारतभूमि के तैंतीस कोटि निवासी संसार भर में तैंतीस कोटि देवताओं के नाम से प्रख्यात हैं। जिस धरती पर वे जन्मते-पलते थे वह ‘स्वर्गादपि गरीयसी’ कही जाती थी। उनके अच्छे क्रिया-कलापों से वातावरण इतना दिव्य बन जाता था कि उसे सतयुग नाम दिया जाना उपयुक्त ही जंचता था, यह समय लम्बी अवधि तक बना रहा। इनके शरीर भी प्रकृति प्रदत्त थे, पर उनके अन्तःकरण में देवत्व कूट-कूटकर भरा था। डिब्बी के भीतर जो वस्तु रखी है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। जिनकी अन्तरात्मा प्रामाणिकता, शालीनता, सेवा और पुरुषार्थ परायणता से सराबोर है उन्हें देवतुल्य ही नहीं वरन् उससे बढ़कर माना जा सकता है। देवता अप्रत्यक्ष होते हैं, मनुहार करने और उपहार देने पर पसीजते हैं। इसके उपरान्त ही उनके वरदान-अनुदान साधकों पर बरसते हैं किन्तु देवमानवों की कृपा-अनुकम्पा अहैतुकी होती है और बिना याचना की प्रतीक्षा किये मेघमाला की तरह बरसती और बसन्त की तरह शोभा-सुषमा से सर्वत्र उल्लास बिखेरती है।
भारत देवभूमि है। स्वर्गलोक के अस्तित्व को चुनौती दिये बिना कहा जा सकता है कि यदि उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो ऐसे महामानवों की उपस्थिति अभी भी जहां-तहां देखी जा सकती है। सतयुग में तो वे साधु-ब्राह्मण के रूप में एक विकसित समुदाय के रूप में ही इस धरित्री की शोभा, सुषमा, संस्कृति एवं समृद्धि का सम्वर्धन करते थे। आज मनुष्य की व्यक्तिगत सामूहिक समस्यायें बेतरह उलझ गई हों, साधन-सामग्री घट गई हों सो बात नहीं है। विज्ञान और कौशल ने साधनों का अतिशय विस्तार किया है, किन्तु व्यक्तित्व की दृष्टि से समुदाय अतिशय बौना हो गया है। कुछ उत्पीड़क हैं, कुछ उत्पीड़ित। कुछ शोषक हैं, कुछ शोषित। कुछ पर्वत की चोटी पर बैठे हैं तो कुछ खाई में गिरकर कराह रहे हैं। इस विषमता को समता में परिणत करने के लिए देवमानवों के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं हो सकता।
पौराणिक कथानकों में अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन के निमित्त अवतारों का प्रकटीकरण होता रहा है। इस अलंकारिक प्रतिपादन का व्यावहारिक स्वरूप यह हो सकता है कि प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता की पक्षधर उदारता सामान्य लोगों जैसी गतिविधियों से उबारकर देव प्रयोजनों में जुट जाने का एकाकी प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सद्भावनापूर्वक अपनाये गये उच्च स्तरीय निर्धारणों को पूरा करने में कर्त्ता की अन्तरात्मा और दैवी शक्तियों की अनुकम्पा समान रूप से, संयुक्त रूप से काम करती है और जो परिणाम सामने आते हैं वे चमत्कारी स्तर के होते हैं। परमार्थी पुरोहितों को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। वस्तुतः वे ही समाज का स्तर, परिस्थितियों का प्रवाह और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते और सफल होकर रहते हैं। समय की पुकार है कि ऐसे उदारचेता उभरें, अपने इर्द-गिर्द के भव-बन्धनों की पकड़ से अपने को उबारें और साथ ही जन-कल्याण की उन प्रवृत्तियों में जुटें जिन्हें प्रकारान्तर से अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापन भी कहा जा सकता है। परिस्थितियों की मांग इतनी प्रबल है कि इससे बच निकलने के लिए कोई बहाना नहीं खोजा जाना चाहिए। सतयुग का माहौल बनाने के लिए भावनाशीलों को संकल्पपूर्वक आगे आना चाहिए, आज की परिस्थितियों में रीति-नीति के अपनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। साधु और ब्राह्मणों को भूसुर-पृथ्वी के देवता कहा जाता है, वे अपनी योग्यता, श्रमशीलता, सम्पदा का न्यूनतम अंश अपने निर्वाह के लिए रखते हैं और शेष को अन्यान्यों को उठाने-बढ़ाने में खर्च करने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। किसी के निवेदन की प्रतीक्षा नहीं करते, बादलों की तरह बिना बुलाये ही सर्वत्र पहुंचते हैं और हर किसी को समुन्नत-सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयास करते हैं—ऐसे ही देवमानवों की संख्या बढ़ने से धरती का वातावरण स्वर्गोपम बनता है।