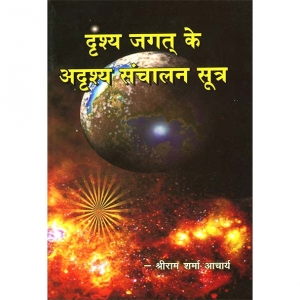दृश्य जगत के अदृश्य संचालन सूत्र 
ईश्वर—एक सत्य एक जीवन दर्शन
Read Scan Version
ईश्वर के अस्तित्व और उसकी सृष्टि सृजन प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुये उपनिषद् के ऋषि ने कहा है कि ‘‘एकोऽहं बहुस्यामः।’’ परमात्मा की एक से अनेक बनने की इच्छा आकांक्षा ही संकल्प रूप में विकसित हुई और यह विश्व ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ। उपनिषद् का कहना है कि ईश्वर ने एक से बहुत बनने की इच्छा की, फलतः यह बहुसंख्यक प्राणी और पदार्थ बन गये। यह चेतन से जड़ की उत्पत्ति हुई। रज शुक्र के संयोग से भ्रूण का आरम्भ होता है। यह भी मानवी चेतना से जड़ शरीर की उत्पत्ति है। जड़ से चेतन उत्पन्न होता है, इसे पानी में काई और मिट्टी में घास उत्पन्न होते समय देखा जा सकता है। गन्दगी में मक्खी मच्छरों का पैदा होना, सड़े हुये फलों में कीड़े उत्पन्न होना यह जड़ से चेतन की उत्पत्ति है।
पदार्थ विज्ञानी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जड़ प्रमुख है। चेतन उसी की एक स्थिति है। ग्रामोफोन का रिकार्ड और उसकी सुई का घर्षण प्रारम्भ होने पर आवाज आरम्भ हो सकती है इसी प्रकार अमुक रसायनों के अमुक स्थिति में—अमुक अनुपात में इकट्ठे होने पर चेतन जीव की स्थिति में जड़ पदार्थ विकसित हो जाते हैं। जीव विज्ञानी अपने प्रतिपादनों में इसी तथ्य को प्रमुखता देते हैं।
लोगों ने प्रश्न किया यदि शारीरिक तत्वों की रासायनिक क्रिया ही मानवीय चेतना के रूप में परिलक्षित होती है तो फिर ज्ञान और विचार क्या हैं? भौतिकतावादी इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में देते हैं—‘‘जिस प्रकार जिगर पित्त उत्पन्न करता है और उससे भूख उत्पन्न होती है उसी प्रकार पदार्थों की प्रतिक्रिया उनके कार्य ही विचार हैं और आंखें जो कुछ देखती हैं (परसेप्शन) वही विचार हैं और ज्ञान के साधन हैं। रासायनिक परिवर्तनों से काम, क्रोध, आकर्षण, प्रेम, स्नेह आदि गुण आविर्भूत होते हैं उनका सम्बन्ध किसी शाश्वत सिद्धान्त से नहीं है। यह एकमात्र भ्रम है और इसी प्रकार लोक मर्यादायें या नैतिकता भी लोगों की सम्मतियां मात्र हैं इनकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
हमारे साथ जो एक विचार प्रणाली काम करती है, ज्ञान, अनुभूति, आकांक्षायें काम करती हैं, प्रेम, आकर्षण स्नेह उद्योग के भाव होते हैं, वह एक कम्प्यूटर में नहीं होते। उसमें जितनी जानकारियां भरदी जाती हैं उस सीमित क्षेत्र से अधिक काम करने की क्षमता उसमें उत्पन्न नहीं हो सकी। मनुष्य जैसा विवेक और आत्म चिन्तन का विकास मनुष्य कृत किसी भी मशीन में नहीं है तो मनुष्य को भी एक रासायनिक संयोग कैसे कहा जा सकता है।
देखना (परसेप्शन) भी रासायनिक गुण नहीं वरन् बाह्य परिस्थितियों पर अवलम्बित ज्ञान है। हमें पता है कि यदि आंखों से प्रकाश न टकराये तो वस्तुयें नहीं देखी जा सकतीं। यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक तो पहुंचता है पर हमारी आंखें खराब हैं इस स्थिति में भी उस वस्तु को देखने से हम वंचित हो जाते हैं। ज्ञान का एक आधार प्रकाश रूप में बाह्य जगत में भी व्याप्त है और अपने भीतर भी दोनों के संयोग से ही ज्ञान की अनुभूति होती है। हम जब नहीं देखते तब भी दूसरे देखते रहते हैं और जब हम देखते हैं तब भी हमारा विचार उस दृश्य वस्तु से परे बहुत दूर का चिन्तन किया करता है यह वह तर्क है जिसके द्वारा हमें यह मानने के लिये विवश होना पड़ता है कि चेतना एक सर्वव्यापी तत्व है और वह रासायनिक चेतना से अधिक समर्थ और शक्तिशाली है।
वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनुमान या विश्वास के बिना हम अधूरे हैं। हम कहां देखते हैं कि ‘‘पृथ्वी चल रही है और सूर्य का चक्कर लगा रहा है’’। हमारी आंखें इतनी छोटी हैं कि विराट् ब्रह्माण्ड (गैलेक्सी) में होने वाली हलचलों को बड़े-बड़े उपकरण लगाकर भी पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। वहां जो कुछ है, जहां-जहां से परिक्रमा पथ बनाते हुए यह ग्रह नक्षत्र चलते हैं उसका ज्ञान हमने अनुमान और विश्वास के आधार पर ही तो प्राप्त किया है यह अनुमान इतने सत्य उतर रहे हैं कि एक सेकेण्ड और एक अंश (डिग्री) समय और कोण का अन्तर किये बिना अन्तरिक्ष यान इन ग्रह नक्षत्रों में उतारे जा रहे हैं। जहां हमारी आंखों का प्रकाश नहीं पहुंचता या जिन स्थानों का प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता वहां की अधिकांश जानकारी का जायजा हम विश्वास और अनुमान के आधार पर ही ले रहे हैं विश्वास एक प्रकार की गणित है और विज्ञान की तरह भावनाओं के क्षेत्र में भी वह सत्य की निरन्तर पुष्टि करता है।
जीव-विज्ञान की प्रचलित धाराओं ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवन और कुछ नहीं जड़ पदार्थों का ही विकसित रूप है।
रासायनिक दृष्टि से जीवन सेल और अणु के एक ही तराजू पर तोला जा सकता है। दोनों में प्रायः समान स्तर में प्राकृतिक नियम काम करते हैं। एकाकी एटम—मालेक्यूल्स और इलेक्ट्रोन्स के बारे में अभी भी वैसी ही खोज जारी है जैसी कि पिछली तीन शताब्दियों में चली रही है। विकिरण—रेडियेशन और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के अभी बहुत से स्पष्टीकरण होने बाकी हैं। जो समझा जा सका है वह अपर्याप्त ही नहीं असन्तोषजनक भी है।
यों कोशिकायें निरन्तर जन्मती-मरती रहती हैं, पर उनमें एक के बार दूसरी में जीवन तत्व का संचार अनवरत रूप से होता रहता है। मृत होने से पूर्व कोशिकायें अपना जीवन तत्व नवजात कोषा को दे जाती हैं, इस प्रकार मरण के साथ ही जीवन की अविच्छिन्न परम्परा निरन्तर चलती रहती है। उन्हें मरणधर्मा होने के साथ-साथ अजर-अमर भी कह सकते हैं। वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया चलते रहने पर भी उनकी अविनाशी सत्ता पर कोई आंच नहीं आती।
नोबुल पुरस्कार विजेता डा. एलेक्सिस कारेल उन दिनों न्यूयार्क के राक फेलर चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र में काम कर रहे थे एक दिन उन्होंने एक मुर्गी के बच्चे के हृदय के जीवित तन्तु का एक रेशा लेकर उसे रक्त एवं प्लाज्मा के घोल में रख दिया। वह रेशा अपने कोष्ठकों की वृद्धि करता हुआ विकास करने लगा। उसे यदि काटा-छांटा न जाता तो वह अपनी वृद्धि करते हुये वजनदार मांस पिण्ड बन जाता। उस प्रयोग से डा. कारेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन जिन तत्वों से बनता है यदि उसे ठीक तरह जाना जा सके और टूट-फूट को सुधारना सम्भव हो सके तो अनन्तकाल तक जीवित रह सकने की सभी सम्भावनायें विद्यमान हैं।
प्रोटोप्लाज्म जीवन का मूल तत्व है। यह तत्व अमरता की विशेषता युक्त है। एक कोश वाला अमीबा प्राणी निरन्तर अपने आपको विभक्त करते हुये वंश वृद्धि करता रहता है। कोई शत्रु उसकी सत्ता ही समाप्त करदे यह दूसरी बात है अन्यथा वह अनन्त काल तक जीवित ही नहीं रहेगा वरन् वंश वृद्धि करते रहने में भी समर्थ रहेगा। रासायनिक सम्मिश्रण से कृत्रिम जीवन उत्पन्न किये जाने की इन दिनों बहुत चर्चा है। छोटे जीवाणु बनाने में ऐसी कुछ सफलता मिली भी है, पर उतने से ही यह दावा करने लगना उचित नहीं कि मनुष्य ने जीवन का—सृजन करने में सफलता प्राप्त करली।
जिन रसायनों से जीवन विनिर्मित किये जाने की चर्चा है क्या उन्हें भी—उनकी प्रकृतिगत विशेषताओं को भी मनुष्य द्वारा बनाया जाना सम्भव है? इस प्रश्न पर वैज्ञानिकों को मौन ही साधे रहना पड़ रहा है। पदार्थ की जो मूल प्रकृति एवं विशेषता है यदि उसे भी मनुष्य कृत प्रयत्नों से नहीं बनाया जा सकता तो इतना ही कहना पड़ेगा कि उसने ढले हुये पुर्जे जोड़कर मशीन खड़ी कर देने जैसा बाल प्रयोजन ही पूरा किया है। ऐसा तो लकड़ी के टुकड़े जोड़कर अक्षर बनाने वाले किन्डर गार्डन कक्षाओं के छात्र भी कर लेते हैं। इतनी भर सफलता से जीव निर्माण जैसे दुस्साध्य कार्य को पूरा कर सकने का दावा करना उपहासास्पद गर्वोक्ति है।
कुछ मशीनें बिजली पैदा करती हैं—कुछ तार बिजली बहाते हैं, पर वे सब बिजली तो नहीं हैं। अमुक रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से जीवन पैदा हो सकता है सो ठीक है, पर उन पदार्थों में जो जीवन पैदा करने की शक्ति है वह अलौकिक एवं सूक्ष्म है। उस शक्ति को उत्पन्न करना जब तक सम्भव न हो तब तक जीवन का सृजेता कहला सकने का गौरव मनुष्य को नहीं मिल सकता।
ब्रह्माण्ड की शक्तियों का और पिण्ड की—मनुष्य की शक्तियों का एकीकरण कहां होता है शरीर शास्त्री इसके लिए सुषुम्ना शीर्षक, मेडुला आवलांगाटा—की ओर इशारा करते हैं। पर वस्तुतः वह वहां है नहीं। मस्तिष्क स्थित ब्रह्मरन्ध्र को ही वह केन्द्र मानना पड़ेगा, जहां ब्राह्मी और जैवी चेतना का समन्वय सम्मिलन होता है। ऊपर के तथ्यों पर विचार करने से यह एकाकी मान्यता ही सीमित नहीं रहती कि जड़ से ही चेतन उत्पन्न होता है इन्हीं तथ्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि चेतन भी जड़ की उत्पत्ति का कारण है। मुर्गी से अण्डा या अण्डे से मुर्गी—नर से नारी या नारी से नर—बीज से वृक्ष या वृक्ष से बीज जैसे प्रश्न अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं। उनका हल न मिलने पर भी किसी को कोई परेशानी नहीं। दोनों को अन्योन्याश्रित मानकर भी काम चल सकता है। ठीक इसी प्रकार जड़ और चेतन में कौन प्रमुख है इस बात पर जोर न देकर यही मानना उचित है कि दोनों एक ही ब्रह्म सत्ता की दो परिस्थितियां मात्र हैं। द्वैत दीखता भर है वस्तुतः यह अद्वैत ही बिखरा पड़ा है।
जड़ में जीवन पाया जाता है यह ठीक है। यह भी ठीक है कि जीवन सत्ता द्वारा जड़ का संचालन होता है। किन्तु यह मान्यता सही नहीं कि जड़ से जीव की उत्पत्ति होती है जीवन जड़ता की एक स्फुरणा मात्र है। अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि जीवन की स्फुरणा से जड़ तत्वों में हलचल उत्पन्न होती है और वह अचेतन होने के बावजूद चेतन दिखाई पड़ता है। मूल सत्ता जड़ की नहीं चेतना की है। चेतना से जड़ का संचालन-परिवर्तन-परिष्कार हो सकता है किन्तु जड़ में न तो जीवन उत्पन्न करने की शक्ति है और न उसे उत्पन्न—प्रभावित करने में समर्थ है। चेतन, जड़ का उपयोगी-उपभोग भर करता है। यही ब्रह्मविद्या की मान्यता परख की कसौटी पर खरी उतरती है। यह सिद्धान्त एक प्रकार से अकाट्य ही है कि—जीव से जीव की उत्पत्ति है। निर्जीव से जीव नहीं बनता है। कृत्रिम जीवन उत्पन्न करने में पिछले दिनों जो सफलता पाई गई है उसकी व्याख्या अधिक से अधिक यही हो सकती है कि अविकसित जीवन स्तर को विकसित जीवन में परिष्कृत किया गया। अभी ऐसा सम्भव नहीं हो सका कि निर्जीव तत्व को जीवित स्तर का बनाया जा सके। संभवतः ऐसा कभी भी न हो सकेगा।
जीवन अविनाशी है। वह सृष्टि के आरम्भ में पैदा हुआ और अन्त तक बना रहेगा। स्थिति के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है। क्योंकि इस जगत का प्रत्येक अणु परिवर्तित होता है हलचलों के कारण ही यहां तरह-तरह की जन्मने, बढ़ने और मरने की गतिविधियां दृश्यमान होती हैं। हलचल रुक जाय तो उसका विकल्प प्रलय—जड़ नीरवता ही हो सकती है। जीवन भी हलचलों से प्रभावित होता है और वह जन्मता, बढ़ता और मरता दीखता है। स्थूल काया की तरह सूक्ष्म कोशिकायें भी जन्मती, बढ़ती और मरती हैं फिर भी उनके भीतर का मूल प्रवाह यथावत् बना रहता है। एक से दूसरे स्थान में—एक से दूसरे रूप में स्थानान्तरण होता दीखता है। यही हलचलों का केन्द्र है। इसी में सृष्टि की शोभा, विशेषता है। इतना सब होते हुए भी जीवन की मूल सत्ता यथावत् अक्षुण्ण बनी रहती है उसका बहिरंग ही बदलता है अन्तरंग को—मूल प्रकृति को अविनाशी सत्ता ही कहा जा सकता है। उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दें सकता—काल भी नहीं।
जड़ से चेतन उत्पन्न हुआ या चेतन से जड़, इस सम्बन्ध में विज्ञान अभी किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं पहुंच सका है। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व को गलत सिद्ध करने वाली नास्तिकवादी मान्यता यह है कि शरीर ही जीव है। शरीर के मरण के साथ-साथ ही जीव का अन्त हो जाता है। शरीर और जीव का पृथक अस्तित्व नहीं है। दोनों एक साथ ही जीते-मरते हैं।
नास्तिक दर्शन के दुष्परिणाम
नास्तिकवाद यदि किसी दार्शनिक चिन्तन तक सीमित रहता तो बाद दूसरी थी पर उसका अत्यन्त दूरगामी प्रभाव हमारी जीवनयापन सम्बन्धी विचारणा एवं क्रिया-प्रक्रिया पर पड़ता है। इसलिए इसे विचार भिन्नता कहकर टाला नहीं जा सकता।
मानवी स्वभाव येनकेन प्रकारेण अधिकाधिक सुख-सुविधा साधनों का संग्रह एवं उपयोग करने का है। कम समय, कम श्रम में अधिक सुख साधन उपलब्ध करने की आतुरता में उचित अनुचित का भेद छूट जाता है। उचित मार्ग से तो अभीष्ट श्रमशीलता और योग्यता के आधार पर ही वस्तुयें मिलती हैं। यदि इस मर्यादा में रुके रहने की गुंजाइश न हो तो गतिविधियों को उस स्तर का बनाना पड़ेगा जैसे पाप, बेईमानी, छल, उत्पीड़न आदि अपराध वर्ग में गिना जा सके। प्रत्यक्ष है कि ईमानदारी की अपेक्षा बेईमानी की नीति अपनाने वाले—स्वल्प समय में अधिक सुख साधन एकत्रित कर लेते हैं। एक की देखा-देखी दूसरे की भी इस प्रचलन का अनुसरण करने की इच्छा होती है और अनैतिक आचरण का प्रवाह द्रुतगति से आगे बढ़ने लगता है। नास्तिकवाद इस प्रवाह को रोकता नहीं वरन् प्रोत्साहित करता है। कहना न होगा कि यदि अपराधी प्रकृति और कृति बढ़ती ही जाय तो आचार संहिता एवं मर्यादा नाम की कोई चीज न रहेगी। स्वेच्छाचार बढ़ेगा और स्वार्थपरता अन्ततः मानव समाज को परस्पर नोंच खाने की स्थिति में लेजाकर पटक देगी फलतः व्यक्ति एवं समाज का सत्यानाशी अहित ही सम्मुख उपस्थित होगा।
कानून की पकड़ से आदमी को बुद्धि कौशल सहज ही बचा सकता है। अपराधों की महामारी अब सर्वजनीन और सर्व व्यापक होती चली जा रही है। पकड़ में कोई विरले ही आते हैं। जो पकड़े जाते हैं वे भी दुर्बल न्याय व्यवस्था का लाभ उठाकर राजदण्ड से बच जाते हैं। समाज में एक तो वैसे ही समर्थ एवं संगठित प्रतिरोध की क्षमता नहीं इस पर भी गुंडावाद का आतंक उसे चुप रहने और सहन करने में ही भलाई मानने के लिए आतंकित करता है। ऐसी दशा में समाज प्रतिरोध का भी भय नहीं रहता सरकारी पकड़ से बचने या पूछने के उपाय तो अब सर्वविदित हो चले हैं इसलिए चतुर लोग उससे डरने की आवश्यकता नहीं समझते। विपत्ति में फंसने से पहले ही आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साधन बना लेते हैं।
अपराधी मनोवृत्ति से बचाने का भावनात्मक अंकुश ही अब तक कारगर होता रहा है। यों उसमें भी भारी शिथिलता आई है फिर भी जितनी रोकथाम आस्तिकता के कारण रही है उसे भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ईश्वर का न्याय, कर्म का फल यदि पूरी तरह मानवी चेतना में से हटा दिया जाय तो फिर उसे आचरण में पूरे उत्साह के साथ प्रवृत्त होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सरकारी नियन्त्रण किसी की बहिरंग गतिविधियों पर ही एक सीमा तक रोकथाम कर सकता है। विचारणा, आकांक्षा एवं अभिरुचि पर तो सरकारी अंकुश भी नहीं चलता। दुष्ट-बुद्धि, दुर्भाव और अशुभ चिन्तन पर रोकथाम तो आत्म-नियन्त्रण से ही हो सकता है। कहना न होगा कि इस आत्म-निग्रह में ईश्वर की उसके न्याय और कर्मफल देने की मान्यता ही कारगर सिद्ध हो सकती है। नास्तिकवादी मान्यता अपनाकर अधिकाधिक सुख-साधन कमाने में फिर कोई बड़ा बन्धन ही नहीं रह जाता। कानून और लोकमत को तो सहज ही बहकाया जा सकता है।
विद्वान वाल्टेयर ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कहा था—‘‘यदि सचमुच ईश्वर नहीं हो तो भी उसका सृजन करना मानवी सुव्यवस्था की दृष्टि से परम आवश्यक है।’’ सत्प्रवृत्तियों को अपनाने और दुष्प्रवृत्तियों से विरत होने की प्रेरणा देने के लिए ही धर्म एवं अध्यात्म का ढांचा खड़ा किया गया है। इन दोनों को ईश्वरवाद की व्याख्या ही धर्म एवं अध्यात्म के क्रियात्मक एवं भावात्मक उत्कृष्टता को समर्पण करने की दृष्टि से की जाती है।
आस्तिकवाद में भी एक भयानक विकृति कुछ समय से ऐसी पनपी है जिसे नास्तिकवाद के समकक्ष ही कह सकते हैं। वह है—छुट-पुट कर्मकाण्डों के आधार पर पाप दंड से छुटकारा मिल जाने का समर्थन। इन दिनों सम्प्रदाय वादियों ने अपने अपने मत-सम्प्रदाय के अनुयायी बनाने और बढ़ाने के लिए एक सस्ता नुस्खा ढूंढ़ निकाला है कि उनके मत के अनुसार बताये पूजा विधान, मन्त्र या क्रियाकृत्य की अत्यन्त सरल विधि पूरी कर लेने से जीवन भर के समस्त पापों के दण्ड से छुटकारा मिल जाता है। यह प्रलोभन इसलिए दिया गया प्रतीत होता है कि पाप दण्ड की कष्टसाध्य प्रक्रिया से सहज ही छुटकारा मिल जाने का भारी लाभ देखकर लोग उनके सम्प्रदाय की रीति-नीति अपना लेंगे। यदि बात इतनी भर होती तो भी क्षम्य थी पर इस मान्यता में एक अत्यन्त भयानक प्रतिक्रिया भी जुड़ी है जिसके कारण वह प्रलोभन व्यक्तिगत चरित्र और समाजगत सुव्यवस्था पर घातक प्रभाव डालता है। मनुष्य पापदण्ड से निर्भय हो जाता है। दुष्कर्म करने का उसे प्रोत्साहन साहस मिलता है। जब अनीति अपना कर भरपूर लाभ उठाया जा सकता है और उनके दण्ड से छुटपुट कर्म-काण्ड का आश्रय ही बचा सकता है तो फिर कोई क्यों अनीति आचरण के लाभ को छोड़ना चाहेगा?
नास्तिकवाद और इस पाप दण्ड से बचाने वाले अनास्तिकवाद का निष्कर्ष एक ही है। नास्तिक इसलिए पाप से निश्चित होता है कि सरकार और समाज को चकमा देने के बाद ईश्वर, परलोक कर्मफल आदि का अतिरिक्त झंझट नहीं रह जाता। ठीक इसी निर्णय पर विकृति चिन्तन से भरा प्रचलित ईश्वरवाद भी पहुंचाता है। इस प्रकार वे बाहर से एक-दूसरे के प्रतिकूल दीखते हुए भी निष्कर्ष एक ही निकालते हैं। पापाचरण के लिए दोनों ही समान रूप से पथ प्रशस्त करते हैं।
एक और प्रश्न पर भी वे दोनों एक मत हैं। पुण्य परमार्थ की आवश्यकता नास्तिकवाद नहीं मानना—क्योंकि इससे धन और समय बर्बाद हो जाता है, जब पुण्य प्रतिफल ही नहीं मिलने वाला है तो प्रत्यक्ष घाटा देने वाले परोपकार जैसे कार्यों को क्यों किया जाय? प्रचलित विकृत अध्यात्मवाद भी यही सिखाता है जब छुट-पुट कर्म-काण्डों के नाम जप आदि से ही अक्षय पुण्य मिल जाता है और स्वर्ग मुक्ति तक का द्वार खुल जाता है तो खर्चीले एवं कष्टसाध्य परमार्थ प्रयोजनों को अपनाने से क्या लाभ? प्रकारान्तर से सेवा सत्कर्मों की निरर्थकता सिद्ध करने में भी यह दोनों ही दर्शन एक मत हैं।
नास्तिकवाद के दुष्परिणामों पर समाज के मूर्धन्य लोग विचार करते रहे हैं और उसे अपनाने पर उत्पन्न होने वाले चरित्र संकट की विभीषिका समझाते रहे हैं। पर न जाने दूसरे उस प्रच्छन्न नास्तिकवाद की ओर विचारशील लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता जो छुट-पुट कर्मकांडों का अतिशयोक्तिपूर्ण महात्म्य बताकर पापदण्ड से निर्भय रहने और निरर्थकता सिद्ध करने में प्रकारान्तर से नास्तिकवाद का सहोदर भाई भी सिद्ध होता है। धर्म, अध्यात्म और ईश्वरवाद के मूल प्रयोजन की यह पृच्छन्न नास्तिकवाद जड़ ही काट रहा है इसलिए उसे भी निरस्त किये जाने की आवश्यकता है।
ईश्वर विश्वास क्यों आवश्यक
ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास, कोरी भावुकता या अविकसित मनोभूमि वाले लोगों को पुरस्कार और दंड के प्रलोभन भय से नीति-मार्ग पर अग्रसर तथा अनीति से विरत करने भर का उपाय नहीं है। नहीं यह काल्पनिक उड़ान ही है। ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण सृष्टि के कण-कण में क्षण-प्रतिक्षण देखा जा सकता है उसके अस्तित्व को स्वीकार भर करने से काम नहीं चलता। सूर्य है और प्रतिदिन निकलता है लेकिन उसके प्रकाश में न बैठा जाय, अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां सभी बंद रखे जायें तो यह मानने भर से सूर्य की उपस्थिति का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
आस्तिकता का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व को मानने न मानने तक ही सीमित नहीं है। उसका असली अर्थ तो ईश्वर की विधि व्यवस्था, नियम मर्यादा और नीति सदाचार की प्रेरणाओं को हृदयंगम करना तथा आचार व्यवहार में उतारना है इस स्थिति को ही ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास कहा जा सकता है।
मनुष्य और समाज पर नैतिक नियमों-मर्यादाओं का अंकुश बनाये रखने के लिए ईश्वर विश्वास ही समर्थ है।
ईश्वर विश्वास की इसलिए भी आवश्यकता है कि उसके सहारे हम जीवन का स्वरूप, लक्ष एवं उपयोग समझने में समर्थ होते हैं। यदि ईश्वरीय विधान को अमान्य ठहरा दिया जाय तो फिर मत्स्यन्याय का ही बोलबाला रहेगा। आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव में बाह्य नियन्त्रण मनुष्य जैसे चतुर प्राणी के लिए कुछ बहुत अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। नियंत्रण के अभाव में सब कुछ अनिश्चित और अविश्वस्त बन जायगा। ऐसी दशा में, हमें आदिमकाल में, वन्य स्थिति में वापिस लौटना पड़ेगा और शरीर निर्वाह करते रहने के लिए पेट प्रजनन एवं सुरक्षा जैसे पशु प्रयत्नों तक सीमित रहना पड़ेगा। ईश्वर विश्वास ने आत्म-नियन्त्रण का पथ-प्रशस्त किया है और उसी आधार पर मानवी, सभ्यता की आचार संहिता का, स्नेह, सहयोग एवं विकास परिष्कार का पथ-प्रशस्त किया है। यदि मान्यता क्षेत्र से ईश्वरीय सत्ता को हटा दिया जाय तो फिर संयम और उदारता जैसी मानवी विशेषताओं को बनाये रहने का कोई दार्शनिक आधार शेष न रह जायगा। तब चिन्तन क्षेत्र में जो उच्छृंखलता प्रवेश करेंगी उसके दुष्परिणाम वैसे ही प्रस्तुत होंगे जैसे कि पुराणकाल की कथा गाथाओं में असुरों के नृशंस क्रिया-कलाप का वर्णन पढ़ने-सुनने को मिलता है।
ईश्वर अन्ध विश्वास नहीं एक तथ्य है। विश्व की व्यवस्था सुनियन्त्रित है, सूर्य, चन्द्र, ग्रह नक्षत्र आदि सभी का उदय-अस्त क्रम अपने ढर्रे पर ठीक तरह चल रहा है, प्रत्येक प्राणी अपने ही जैसी सन्तान उत्पन्न करता है और हर बीज अपनी ही जाति का पौधा उत्पन्न करता है। अणु-परमाणुओं से लेकर समुद्र, पर्वतों तक की उत्पादन वृद्धि एवं मरण का क्रिया-कलाप अपने ढंग से ठीक प्रकार चल रहा है। शरीर और मस्तिष्क की संरचना और कार्यशैली देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतनी सुव्यवस्थित कार्यपद्धति बिना किसी चेतना शक्ति के अनायास ही नहीं चल सकती। उस नियन्ता का अस्तित्व जड़ और चेतन के दोनों क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष की दोनों कसौटियों पर पूर्णतया खरा सिद्ध होता है। वह समय चला गया जब अधकचरे विज्ञान के नाम पर संसार क्रम को स्वसंचालित और प्राणी को चलता-फिरता पौधा मात्र ठहराया गया था। अब पदार्थ विज्ञान और चेतन विज्ञान में इतनी प्रौढ़ता आ गई है कि वे नियामक चेतना शक्ति के अस्तित्व को बिना किसी आना-कानी के स्वीकार कर सकें। कर्मफल की व्यवस्था भी उसी नियन्त्रण के अन्तर्गत आती है। समाज और शासन द्वारा दण्ड, पुरस्कार की व्यवस्था है। ईश्वरीय न्याय में भी सत्कर्मों और दुष्कर्मों के लिए समुचित पुरस्कार और दण्ड का विधान है। देर तो मुकदमे होने में भी लगती है और बीज बोने के बाद फसल काटने में भी। इस व्यवस्था को स्थूल बुद्धि समझ नहीं पाती। सत्कर्मों का फल तत्काल न मिलने पर लोग अधीर होने लगते हैं और दुष्कर्मों का तात्कालिक लाभ देखकर उनके लिए आतुरता प्रकट करते हैं। इन भूलभुलैयों में भटका व्यक्ति अपना और समाज का भविष्य अन्धकारमय बनाता है और वर्तमान को अवांछनीयताओं से भर देता है। इस गड़बड़ी की रोकथाम में ईश्वर विश्वास से भारी सहायता मिलती है और व्यक्तिगत चरित्र-निष्ठा एवं समाजगत सुव्यवस्था का आधार सुदृढ़ बना रहता है। इन्हीं सब दूरगामी परिणामों को देखते हुए तत्वज्ञानियों ने ईश्वर विश्वास को दृढ़तापूर्वक अपनाये रहने के लिए जन साधारण को विशेष रूप से प्रेरणा दी है। वह आधार दुर्बल न होने पाये, हर रोज स्मृतिपटल पर जमा रहे इसलिए साधना, उपासना के धर्मकृत्यों का सुविस्तृत विधि-विधान विनिर्मित किया है। इन्हें अपनाकर मनुष्य दिव्यसत्ता को अपने भीतर बाहर विद्यमान देखता है और कुमार्ग से विरत रहकर सन्मार्ग पर चलने का अधिक उत्साह के साथ प्रयत्न करता है। ईश्वर विश्वास के फलस्वरूप पशु प्रवृत्तियों के नियन्त्रण में भारी सहायता मिलती है और व्यक्ति तथा समाज का स्तर सन्तुलित बनाये रहने का प्रयोजन बहुत अंशों तक पूरा होता है। नास्तिकता अपनाकर विश्व-शान्ति का—मानवी उत्कृष्टता का आधार ही डगमगाने लगेगा, इसलिए तत्वदर्शियों ने आध्यात्मिक अनास्था नास्तिकता की कठोर शब्दों में भर्त्सना की है।
जीवन-दर्शन को ईश्वर विश्वास से उच्चस्तरीय प्रेरणा मिलती है। संसार के सभी प्राणी ईश्वर पुत्र हैं। कोई न्यायप्रिय, निष्पक्ष पिता अपनी सभी सन्तानों को लगभग समान स्नेह और समान अनुदान देने का प्रयत्न करता है। ईश्वर ने अन्य प्राणियों को मात्र शरीर निर्वाह जितनी बुद्धि और सुविधा दी तथा मनुष्य को बोलने, सोचने, पढ़ने, कमाने, बनाने आदि की अनेकों विभूतियां दी हैं। अन्य प्राणियों की और मनुष्यों की स्थिति की तुलना करने पर जमीन-आसमान जैसा अन्तर दिखाई पड़ता है। इसमें पक्षपात और अनीति का आक्षेप ईश्वर पर लगता है। जब सामान्य प्राणी अपनी सन्तान को समान स्नेह, सहयोग देते हैं तो फिर ईश्वर ने इतना अन्तर किसलिए रखा? एक को इतना ऊंचा और दूसरे को इतना नीचा कैसे रखा? इस विभेद को समझने में प्रत्येक विवेक सम्पन्न व्यक्ति को भारी उलझन का सामना करना पड़ता है। तत्वदर्शी विवेक बुद्धि इस विभेद के अन्तर का कारण भली प्रकार स्पष्ट कर देती है। मनुष्य को अपने वरिष्ठ सहकारी ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सृजा गया है। उसके कन्धों पर सृष्टि को अधिक सुन्दर, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके लिए उसे विशिष्ठ साधन उसी विशिष्ठ प्रयोजन के लिए अमानत के रूप में दिये गये हैं। मिनिस्टरों को सामान्य कर्मचारियों की तुलना में सरकार अधिक सुविधा साधन इसलिए देती है कि उनकी सहायता से वे अपने विशिष्ठ उत्तरदायित्वों का निर्वाह सुविधापूर्वक कर सकें। यह सुविधाएं उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरन् जन-सेवा के लिए दी जाती हैं। बैंक के खजानची के हाथ में बहुत-सा पैसा रहता है यह उसके निजी उपभोग के लिए बैंक प्रयोजन के लिए अमानत रूप में रहता है। निजी प्रयोजन के लिए तो क्या मिनिस्टर, क्या खजानची सभी को सीमित सुविधा मिलती हैं। अत्यधिक साधन जो उनके हाथ में रहते हैं उन्हें वे निर्दिष्ट कार्यों में ही खर्च कर सकते हैं। निजी कार्यों में उपभोग करने लगें तो यह दण्डनीय अपराध होगा।
ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास सामान्य प्राणियों को उपलब्ध शरीर निर्वाह भर के साधनों से अतिरिक्त जो कुछ भी श्रम, समय, बुद्धि, वैभव, धन, प्रभाव, प्रतिभा आदि की विभूतियां हैं, वह सभी लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए मिली हुई सार्वजनिक सम्पत्ति है। शरीर रक्षा एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए औसत नागरिक-स्तर का निर्वाह कर लेने के अतिरिक्त मनुष्य के पास जो कुछ बचता है उसकी एक-एक बूंद उसे लोक-कल्याण के लिए नियोजित करनी चाहिए। इसी में ईश्वरीय अनुदान और मानवी गरिमा की सार्थकता है। प्रत्येक आस्तिक को सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन की गरिमा, उपयोगिता और जिम्मेदारी समझनी चाहिए तथा उसी के अनुरूप अपने चिन्तन तथा कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। अपनी विशेषताओं का उपयोग इसी महान प्रयोजन के लिए करना चाहिए।
जीवन-दर्शन की यह उत्कृष्ट प्रेरणा ईश्वर विश्वास के आधार पर ही मिलती है। जीवन क्या है, क्यों है, उसका लक्ष्य एवं उपयोग क्या है? इन प्रश्नों का समाधान मात्र आस्तिकता के साथ जुड़ी हुई दिव्य दूरदर्शिता के आधार पर ही मिलता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित मनुष्य संकीर्ण स्वार्थपरता से—वासना, तृष्णा के भव-बन्धनों से छुटकारा पाकर आत्म-निर्माण की ओर—आत्म विस्तार की ओर—आत्म-विकास की ओर अग्रसर होता है और ऐतिहासिक महामानवों जैसी देव भूमिका अपनाने के लिए अग्रसर होता है। व्यक्ति और समाज के कल्याण के महान् आधार खड़े करने वाली यह एक बहुत बड़ी दार्शनिक उपलब्धि है। यदि आस्तिकता का यही स्वरूप समझा जा सके और जीवन-दर्शन के साथ उसे ठीक प्रकार जोड़ा जा सके तो निश्चय ही मनुष्य में देवत्व का उदय और इसी धरती पर स्वर्ग का अवतरण सम्भव हो सकता है। यही तो ईश्वर द्वारा मनुष्य सृजन का एकमात्र उद्देश्य है।
सृष्टि के सभी प्राणी एक पिता के पुत्र होने के नाते सहोदर भाई हैं और वे परस्पर एक-दूसरे का स्नेह, सहयोग पाने के अधिकारी हैं। आस्तिकता यही मान्यता अपनाने के लिए प्रत्येक विचारशील को प्रेरणा देती है। इसका अनुसरण करके प्राणिमात्र के बीच आत्मीयता की भावना विकसित हो सकती है और उसके आधार पर एक-दूसरे के दुःख-दर्द को अपना समझने एवं उदार व्यवहार करने की आकांक्षा प्रबल हो सकती है। विश्व-कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार की भावनात्मक स्थापनाएं अतीव श्रेयस्कर परिणाम प्रस्तुत कर सकती हैं। कहना न होगा कि यह दृष्टिकोण हर दृष्टि से—हर क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य की भूमिका प्रस्तुत कर सकने वाला सिद्ध हो सकता है। ईश्वर विश्वास के कल्पवृक्ष पर तीन फल लगते बताये गये हैं—(1) सिद्धि (2) स्वर्ग (3) मुक्ति। सिद्धि का अर्थ है प्रतिभावान परिष्कृत व्यक्तित्व और उसके आधार पर बन पड़ने वाले प्रबल पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया अनेकानेक भौतिक सफलताओं के रूप में प्राप्त होना। स्पष्ट है कि चिरस्थायी और प्रशंसनीय सफलताएं गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता के फलस्वरूप ही उपलब्ध होती हैं। मनुष्य को दुष्प्रवृत्तियों से विरत करने और सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श कर्तृत्व अपनाना पड़ता है। यह सभी आधार आस्तिकतावादी दर्शन में कूट-कूटकर भरे हैं। आज का विकृत अध्यात्म-दर्शन तो मनुष्य को उलटे भ्रम-जंजालों में फंसाकर सामान्य व्यक्तियों से भी गई-गुजरी स्थिति में धकेलता है, पर यदि उसका यथार्थ स्वरूप विदित हो तो उसे अपनाने का साहस बन पड़े तो निश्चित रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। जहां यह सफलता मिली वहां अन्य सफलतायें हाथ बांधकर सामने खड़ी दिखाई पड़ेंगीं। महामानवों द्वारा प्रस्तुत किये गये चमत्कारी क्रिया-कलाप इसी तथ्य की साक्षी देते हैं। इसी को सिद्धि करते हैं। अध्यात्मवादी आस्तिक व्यक्ति चमत्कारी सिद्धियों से भरे-पूरे होते हैं। इस मान्यता को उपरोक्त आधार पर अक्षरशः सही ठहराया जा सकता है। किन्तु यदि सिद्धि का मतलब बाजीगरी जैसी अचम्भे में डालने वाली करामातें समझा जाय तो यही कहा जायगा कि वैसा दिखाने वाले धूर्त और देखने के लिए लालायित व्यक्ति मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।
आस्तिकता के कल्पवृक्ष पर लगने वाला दूसरा फल है—स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ है—परिष्कृत गुणग्राही विधायक दृष्टिकोण। परिष्कृत दृष्टिकोण होने पर अभावग्रस्त दरिद्र मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मनुष्य जीवन अपने आप में इतना पूर्ण है कि उस सम्पत्ति को संसार की समस्त एकत्रित सम्पदा की तुलना में भी अधिक भारी माना जा सकता है। शरीर यात्रा के अनिवार्य साधन प्रायः हर किसी को मिले होते हैं, अभाव तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकने के कारण ही प्रतीत होता है। अभावों की, कठिनाइयों की, विरोधियों की लिस्ट फाड़ फेंकी जाय और उपलब्धियों, सुविधाओं, सहयोगियों की सूची नये सिरे से बनाई जाय तो प्रतीत होगा कि कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दरिद्र चला गया, उसके स्थान पर वैभव आ विराजा। छिद्रान्वेषण की आदत हटाकर गुण ग्राहकता अपनाई जाय तो प्रतीत होगा कि इस संसार में ईश्वरीय उद्यान की—नन्दन वन की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। स्वर्ग इसी विधायक दृष्टिकोण का नाम है—जिसे अपनाकर अपनी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की देव सम्पदा को हर घड़ी प्रसन्न रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। स्वर्ग और नरक कोई क्षेत्र नहीं वरन् लोक हैं। लोक का अर्थ है दृष्टिकोण। निकृष्ट चिन्तन की प्रतिक्रिया नारकीय दुःख दारिद्रय से भरी हुई होती है और उत्कृष्टता भरी विचारणाओं का प्रतिफल स्वर्ग जैसी सुख-शान्ति प्रस्तुत करता रहता है। ईश्वर विश्वास की राह पर चलता हुआ मनुष्य स्वर्गीय वातावरण प्रस्तुत करता है, उसमें स्वयं रहते हुए आनन्द अनुभव करता है और समीपवर्ती क्षेत्र को उसी प्रकाश से दीप्तिवान बनाता है।
आस्तिकता का तीसरा प्रतिफल है—मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है—अवांछनीय भव-बन्धनों से छूटना। अपनी दुष्प्रवृत्ति, मूढ़ मान्यताएं एवं विकृत आकांक्षाएं ही वस्तुतः सर्वनाश करने वाली पिशाचिनी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, चिंता, भय, दैन्य जैसे मनोविकार ही व्यक्तित्व को गिराते, गलाते, जलाते हैं। आधि और व्याधि इन्हीं के आमन्त्रण पर आक्रमण करती हैं। आस्तिकता इन्हीं दुर्बलताओं से जूझने की प्रेरणा भरती है। सारा साधना शास्त्र इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ने, खदेड़ने की पृष्ठभूमि विनिर्मित करने के लिए खड़ा किया गया है। इनसे छुटकारा पान पर देवत्व द्रुतगति से उभरता है और अपनी स्वतन्त्र सत्ता का उल्लास भरा अनुभव होता है।
मनुष्य कितने ही दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों, पक्षपातों, प्रचलनों, अनुकरणों से घिरा बंधा कंटकाकीर्ण राह पर घिसटता रहता है। स्वतंत्र चिन्तन की विवेक दृष्टि उसे कदाचित ही मिल पाती है। यदि वह मिली होती तो निश्चय ही औचित्य को प्रश्रय दिया गया होता और तथाकथित मित्र, परिचित क्या कहते हैं? इसकी पूर्णतया उपेक्षा करके विवेक के प्रकाश में कदम बढ़ाने का साहस संजोया होता। महामानव इसी सत्साहस के बल पर स्वयं धन्य बने हैं और अपने युग को—क्षेत्र को धन्य बनाया है। जीवन-मुक्त पुरुष अवांछनीय चिन्तन से मुक्त होते हैं और आत्मिक स्वतन्त्रता का आनन्द लेते हैं। स्पष्ट है कि ईश्वर भक्तों को संयमी, स्वार्थपरता से रहित, लोकोपयोगी ब्राह्मण और साधु स्तर का जीवन जीना पड़ता है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ईश्वर विश्वास अपनाकर हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं और उसे पाकर रहते हैं।
पदार्थ विज्ञानी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जड़ प्रमुख है। चेतन उसी की एक स्थिति है। ग्रामोफोन का रिकार्ड और उसकी सुई का घर्षण प्रारम्भ होने पर आवाज आरम्भ हो सकती है इसी प्रकार अमुक रसायनों के अमुक स्थिति में—अमुक अनुपात में इकट्ठे होने पर चेतन जीव की स्थिति में जड़ पदार्थ विकसित हो जाते हैं। जीव विज्ञानी अपने प्रतिपादनों में इसी तथ्य को प्रमुखता देते हैं।
लोगों ने प्रश्न किया यदि शारीरिक तत्वों की रासायनिक क्रिया ही मानवीय चेतना के रूप में परिलक्षित होती है तो फिर ज्ञान और विचार क्या हैं? भौतिकतावादी इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में देते हैं—‘‘जिस प्रकार जिगर पित्त उत्पन्न करता है और उससे भूख उत्पन्न होती है उसी प्रकार पदार्थों की प्रतिक्रिया उनके कार्य ही विचार हैं और आंखें जो कुछ देखती हैं (परसेप्शन) वही विचार हैं और ज्ञान के साधन हैं। रासायनिक परिवर्तनों से काम, क्रोध, आकर्षण, प्रेम, स्नेह आदि गुण आविर्भूत होते हैं उनका सम्बन्ध किसी शाश्वत सिद्धान्त से नहीं है। यह एकमात्र भ्रम है और इसी प्रकार लोक मर्यादायें या नैतिकता भी लोगों की सम्मतियां मात्र हैं इनकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
हमारे साथ जो एक विचार प्रणाली काम करती है, ज्ञान, अनुभूति, आकांक्षायें काम करती हैं, प्रेम, आकर्षण स्नेह उद्योग के भाव होते हैं, वह एक कम्प्यूटर में नहीं होते। उसमें जितनी जानकारियां भरदी जाती हैं उस सीमित क्षेत्र से अधिक काम करने की क्षमता उसमें उत्पन्न नहीं हो सकी। मनुष्य जैसा विवेक और आत्म चिन्तन का विकास मनुष्य कृत किसी भी मशीन में नहीं है तो मनुष्य को भी एक रासायनिक संयोग कैसे कहा जा सकता है।
देखना (परसेप्शन) भी रासायनिक गुण नहीं वरन् बाह्य परिस्थितियों पर अवलम्बित ज्ञान है। हमें पता है कि यदि आंखों से प्रकाश न टकराये तो वस्तुयें नहीं देखी जा सकतीं। यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक तो पहुंचता है पर हमारी आंखें खराब हैं इस स्थिति में भी उस वस्तु को देखने से हम वंचित हो जाते हैं। ज्ञान का एक आधार प्रकाश रूप में बाह्य जगत में भी व्याप्त है और अपने भीतर भी दोनों के संयोग से ही ज्ञान की अनुभूति होती है। हम जब नहीं देखते तब भी दूसरे देखते रहते हैं और जब हम देखते हैं तब भी हमारा विचार उस दृश्य वस्तु से परे बहुत दूर का चिन्तन किया करता है यह वह तर्क है जिसके द्वारा हमें यह मानने के लिये विवश होना पड़ता है कि चेतना एक सर्वव्यापी तत्व है और वह रासायनिक चेतना से अधिक समर्थ और शक्तिशाली है।
वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनुमान या विश्वास के बिना हम अधूरे हैं। हम कहां देखते हैं कि ‘‘पृथ्वी चल रही है और सूर्य का चक्कर लगा रहा है’’। हमारी आंखें इतनी छोटी हैं कि विराट् ब्रह्माण्ड (गैलेक्सी) में होने वाली हलचलों को बड़े-बड़े उपकरण लगाकर भी पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। वहां जो कुछ है, जहां-जहां से परिक्रमा पथ बनाते हुए यह ग्रह नक्षत्र चलते हैं उसका ज्ञान हमने अनुमान और विश्वास के आधार पर ही तो प्राप्त किया है यह अनुमान इतने सत्य उतर रहे हैं कि एक सेकेण्ड और एक अंश (डिग्री) समय और कोण का अन्तर किये बिना अन्तरिक्ष यान इन ग्रह नक्षत्रों में उतारे जा रहे हैं। जहां हमारी आंखों का प्रकाश नहीं पहुंचता या जिन स्थानों का प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता वहां की अधिकांश जानकारी का जायजा हम विश्वास और अनुमान के आधार पर ही ले रहे हैं विश्वास एक प्रकार की गणित है और विज्ञान की तरह भावनाओं के क्षेत्र में भी वह सत्य की निरन्तर पुष्टि करता है।
जीव-विज्ञान की प्रचलित धाराओं ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवन और कुछ नहीं जड़ पदार्थों का ही विकसित रूप है।
रासायनिक दृष्टि से जीवन सेल और अणु के एक ही तराजू पर तोला जा सकता है। दोनों में प्रायः समान स्तर में प्राकृतिक नियम काम करते हैं। एकाकी एटम—मालेक्यूल्स और इलेक्ट्रोन्स के बारे में अभी भी वैसी ही खोज जारी है जैसी कि पिछली तीन शताब्दियों में चली रही है। विकिरण—रेडियेशन और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के अभी बहुत से स्पष्टीकरण होने बाकी हैं। जो समझा जा सका है वह अपर्याप्त ही नहीं असन्तोषजनक भी है।
यों कोशिकायें निरन्तर जन्मती-मरती रहती हैं, पर उनमें एक के बार दूसरी में जीवन तत्व का संचार अनवरत रूप से होता रहता है। मृत होने से पूर्व कोशिकायें अपना जीवन तत्व नवजात कोषा को दे जाती हैं, इस प्रकार मरण के साथ ही जीवन की अविच्छिन्न परम्परा निरन्तर चलती रहती है। उन्हें मरणधर्मा होने के साथ-साथ अजर-अमर भी कह सकते हैं। वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया चलते रहने पर भी उनकी अविनाशी सत्ता पर कोई आंच नहीं आती।
नोबुल पुरस्कार विजेता डा. एलेक्सिस कारेल उन दिनों न्यूयार्क के राक फेलर चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र में काम कर रहे थे एक दिन उन्होंने एक मुर्गी के बच्चे के हृदय के जीवित तन्तु का एक रेशा लेकर उसे रक्त एवं प्लाज्मा के घोल में रख दिया। वह रेशा अपने कोष्ठकों की वृद्धि करता हुआ विकास करने लगा। उसे यदि काटा-छांटा न जाता तो वह अपनी वृद्धि करते हुये वजनदार मांस पिण्ड बन जाता। उस प्रयोग से डा. कारेल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन जिन तत्वों से बनता है यदि उसे ठीक तरह जाना जा सके और टूट-फूट को सुधारना सम्भव हो सके तो अनन्तकाल तक जीवित रह सकने की सभी सम्भावनायें विद्यमान हैं।
प्रोटोप्लाज्म जीवन का मूल तत्व है। यह तत्व अमरता की विशेषता युक्त है। एक कोश वाला अमीबा प्राणी निरन्तर अपने आपको विभक्त करते हुये वंश वृद्धि करता रहता है। कोई शत्रु उसकी सत्ता ही समाप्त करदे यह दूसरी बात है अन्यथा वह अनन्त काल तक जीवित ही नहीं रहेगा वरन् वंश वृद्धि करते रहने में भी समर्थ रहेगा। रासायनिक सम्मिश्रण से कृत्रिम जीवन उत्पन्न किये जाने की इन दिनों बहुत चर्चा है। छोटे जीवाणु बनाने में ऐसी कुछ सफलता मिली भी है, पर उतने से ही यह दावा करने लगना उचित नहीं कि मनुष्य ने जीवन का—सृजन करने में सफलता प्राप्त करली।
जिन रसायनों से जीवन विनिर्मित किये जाने की चर्चा है क्या उन्हें भी—उनकी प्रकृतिगत विशेषताओं को भी मनुष्य द्वारा बनाया जाना सम्भव है? इस प्रश्न पर वैज्ञानिकों को मौन ही साधे रहना पड़ रहा है। पदार्थ की जो मूल प्रकृति एवं विशेषता है यदि उसे भी मनुष्य कृत प्रयत्नों से नहीं बनाया जा सकता तो इतना ही कहना पड़ेगा कि उसने ढले हुये पुर्जे जोड़कर मशीन खड़ी कर देने जैसा बाल प्रयोजन ही पूरा किया है। ऐसा तो लकड़ी के टुकड़े जोड़कर अक्षर बनाने वाले किन्डर गार्डन कक्षाओं के छात्र भी कर लेते हैं। इतनी भर सफलता से जीव निर्माण जैसे दुस्साध्य कार्य को पूरा कर सकने का दावा करना उपहासास्पद गर्वोक्ति है।
कुछ मशीनें बिजली पैदा करती हैं—कुछ तार बिजली बहाते हैं, पर वे सब बिजली तो नहीं हैं। अमुक रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से जीवन पैदा हो सकता है सो ठीक है, पर उन पदार्थों में जो जीवन पैदा करने की शक्ति है वह अलौकिक एवं सूक्ष्म है। उस शक्ति को उत्पन्न करना जब तक सम्भव न हो तब तक जीवन का सृजेता कहला सकने का गौरव मनुष्य को नहीं मिल सकता।
ब्रह्माण्ड की शक्तियों का और पिण्ड की—मनुष्य की शक्तियों का एकीकरण कहां होता है शरीर शास्त्री इसके लिए सुषुम्ना शीर्षक, मेडुला आवलांगाटा—की ओर इशारा करते हैं। पर वस्तुतः वह वहां है नहीं। मस्तिष्क स्थित ब्रह्मरन्ध्र को ही वह केन्द्र मानना पड़ेगा, जहां ब्राह्मी और जैवी चेतना का समन्वय सम्मिलन होता है। ऊपर के तथ्यों पर विचार करने से यह एकाकी मान्यता ही सीमित नहीं रहती कि जड़ से ही चेतन उत्पन्न होता है इन्हीं तथ्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि चेतन भी जड़ की उत्पत्ति का कारण है। मुर्गी से अण्डा या अण्डे से मुर्गी—नर से नारी या नारी से नर—बीज से वृक्ष या वृक्ष से बीज जैसे प्रश्न अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं। उनका हल न मिलने पर भी किसी को कोई परेशानी नहीं। दोनों को अन्योन्याश्रित मानकर भी काम चल सकता है। ठीक इसी प्रकार जड़ और चेतन में कौन प्रमुख है इस बात पर जोर न देकर यही मानना उचित है कि दोनों एक ही ब्रह्म सत्ता की दो परिस्थितियां मात्र हैं। द्वैत दीखता भर है वस्तुतः यह अद्वैत ही बिखरा पड़ा है।
जड़ में जीवन पाया जाता है यह ठीक है। यह भी ठीक है कि जीवन सत्ता द्वारा जड़ का संचालन होता है। किन्तु यह मान्यता सही नहीं कि जड़ से जीव की उत्पत्ति होती है जीवन जड़ता की एक स्फुरणा मात्र है। अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि जीवन की स्फुरणा से जड़ तत्वों में हलचल उत्पन्न होती है और वह अचेतन होने के बावजूद चेतन दिखाई पड़ता है। मूल सत्ता जड़ की नहीं चेतना की है। चेतना से जड़ का संचालन-परिवर्तन-परिष्कार हो सकता है किन्तु जड़ में न तो जीवन उत्पन्न करने की शक्ति है और न उसे उत्पन्न—प्रभावित करने में समर्थ है। चेतन, जड़ का उपयोगी-उपभोग भर करता है। यही ब्रह्मविद्या की मान्यता परख की कसौटी पर खरी उतरती है। यह सिद्धान्त एक प्रकार से अकाट्य ही है कि—जीव से जीव की उत्पत्ति है। निर्जीव से जीव नहीं बनता है। कृत्रिम जीवन उत्पन्न करने में पिछले दिनों जो सफलता पाई गई है उसकी व्याख्या अधिक से अधिक यही हो सकती है कि अविकसित जीवन स्तर को विकसित जीवन में परिष्कृत किया गया। अभी ऐसा सम्भव नहीं हो सका कि निर्जीव तत्व को जीवित स्तर का बनाया जा सके। संभवतः ऐसा कभी भी न हो सकेगा।
जीवन अविनाशी है। वह सृष्टि के आरम्भ में पैदा हुआ और अन्त तक बना रहेगा। स्थिति के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है। क्योंकि इस जगत का प्रत्येक अणु परिवर्तित होता है हलचलों के कारण ही यहां तरह-तरह की जन्मने, बढ़ने और मरने की गतिविधियां दृश्यमान होती हैं। हलचल रुक जाय तो उसका विकल्प प्रलय—जड़ नीरवता ही हो सकती है। जीवन भी हलचलों से प्रभावित होता है और वह जन्मता, बढ़ता और मरता दीखता है। स्थूल काया की तरह सूक्ष्म कोशिकायें भी जन्मती, बढ़ती और मरती हैं फिर भी उनके भीतर का मूल प्रवाह यथावत् बना रहता है। एक से दूसरे स्थान में—एक से दूसरे रूप में स्थानान्तरण होता दीखता है। यही हलचलों का केन्द्र है। इसी में सृष्टि की शोभा, विशेषता है। इतना सब होते हुए भी जीवन की मूल सत्ता यथावत् अक्षुण्ण बनी रहती है उसका बहिरंग ही बदलता है अन्तरंग को—मूल प्रकृति को अविनाशी सत्ता ही कहा जा सकता है। उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दें सकता—काल भी नहीं।
जड़ से चेतन उत्पन्न हुआ या चेतन से जड़, इस सम्बन्ध में विज्ञान अभी किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं पहुंच सका है। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व को गलत सिद्ध करने वाली नास्तिकवादी मान्यता यह है कि शरीर ही जीव है। शरीर के मरण के साथ-साथ ही जीव का अन्त हो जाता है। शरीर और जीव का पृथक अस्तित्व नहीं है। दोनों एक साथ ही जीते-मरते हैं।
नास्तिक दर्शन के दुष्परिणाम
नास्तिकवाद यदि किसी दार्शनिक चिन्तन तक सीमित रहता तो बाद दूसरी थी पर उसका अत्यन्त दूरगामी प्रभाव हमारी जीवनयापन सम्बन्धी विचारणा एवं क्रिया-प्रक्रिया पर पड़ता है। इसलिए इसे विचार भिन्नता कहकर टाला नहीं जा सकता।
मानवी स्वभाव येनकेन प्रकारेण अधिकाधिक सुख-सुविधा साधनों का संग्रह एवं उपयोग करने का है। कम समय, कम श्रम में अधिक सुख साधन उपलब्ध करने की आतुरता में उचित अनुचित का भेद छूट जाता है। उचित मार्ग से तो अभीष्ट श्रमशीलता और योग्यता के आधार पर ही वस्तुयें मिलती हैं। यदि इस मर्यादा में रुके रहने की गुंजाइश न हो तो गतिविधियों को उस स्तर का बनाना पड़ेगा जैसे पाप, बेईमानी, छल, उत्पीड़न आदि अपराध वर्ग में गिना जा सके। प्रत्यक्ष है कि ईमानदारी की अपेक्षा बेईमानी की नीति अपनाने वाले—स्वल्प समय में अधिक सुख साधन एकत्रित कर लेते हैं। एक की देखा-देखी दूसरे की भी इस प्रचलन का अनुसरण करने की इच्छा होती है और अनैतिक आचरण का प्रवाह द्रुतगति से आगे बढ़ने लगता है। नास्तिकवाद इस प्रवाह को रोकता नहीं वरन् प्रोत्साहित करता है। कहना न होगा कि यदि अपराधी प्रकृति और कृति बढ़ती ही जाय तो आचार संहिता एवं मर्यादा नाम की कोई चीज न रहेगी। स्वेच्छाचार बढ़ेगा और स्वार्थपरता अन्ततः मानव समाज को परस्पर नोंच खाने की स्थिति में लेजाकर पटक देगी फलतः व्यक्ति एवं समाज का सत्यानाशी अहित ही सम्मुख उपस्थित होगा।
कानून की पकड़ से आदमी को बुद्धि कौशल सहज ही बचा सकता है। अपराधों की महामारी अब सर्वजनीन और सर्व व्यापक होती चली जा रही है। पकड़ में कोई विरले ही आते हैं। जो पकड़े जाते हैं वे भी दुर्बल न्याय व्यवस्था का लाभ उठाकर राजदण्ड से बच जाते हैं। समाज में एक तो वैसे ही समर्थ एवं संगठित प्रतिरोध की क्षमता नहीं इस पर भी गुंडावाद का आतंक उसे चुप रहने और सहन करने में ही भलाई मानने के लिए आतंकित करता है। ऐसी दशा में समाज प्रतिरोध का भी भय नहीं रहता सरकारी पकड़ से बचने या पूछने के उपाय तो अब सर्वविदित हो चले हैं इसलिए चतुर लोग उससे डरने की आवश्यकता नहीं समझते। विपत्ति में फंसने से पहले ही आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साधन बना लेते हैं।
अपराधी मनोवृत्ति से बचाने का भावनात्मक अंकुश ही अब तक कारगर होता रहा है। यों उसमें भी भारी शिथिलता आई है फिर भी जितनी रोकथाम आस्तिकता के कारण रही है उसे भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ईश्वर का न्याय, कर्म का फल यदि पूरी तरह मानवी चेतना में से हटा दिया जाय तो फिर उसे आचरण में पूरे उत्साह के साथ प्रवृत्त होने से कोई रोक नहीं सकेगा। सरकारी नियन्त्रण किसी की बहिरंग गतिविधियों पर ही एक सीमा तक रोकथाम कर सकता है। विचारणा, आकांक्षा एवं अभिरुचि पर तो सरकारी अंकुश भी नहीं चलता। दुष्ट-बुद्धि, दुर्भाव और अशुभ चिन्तन पर रोकथाम तो आत्म-नियन्त्रण से ही हो सकता है। कहना न होगा कि इस आत्म-निग्रह में ईश्वर की उसके न्याय और कर्मफल देने की मान्यता ही कारगर सिद्ध हो सकती है। नास्तिकवादी मान्यता अपनाकर अधिकाधिक सुख-साधन कमाने में फिर कोई बड़ा बन्धन ही नहीं रह जाता। कानून और लोकमत को तो सहज ही बहकाया जा सकता है।
विद्वान वाल्टेयर ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कहा था—‘‘यदि सचमुच ईश्वर नहीं हो तो भी उसका सृजन करना मानवी सुव्यवस्था की दृष्टि से परम आवश्यक है।’’ सत्प्रवृत्तियों को अपनाने और दुष्प्रवृत्तियों से विरत होने की प्रेरणा देने के लिए ही धर्म एवं अध्यात्म का ढांचा खड़ा किया गया है। इन दोनों को ईश्वरवाद की व्याख्या ही धर्म एवं अध्यात्म के क्रियात्मक एवं भावात्मक उत्कृष्टता को समर्पण करने की दृष्टि से की जाती है।
आस्तिकवाद में भी एक भयानक विकृति कुछ समय से ऐसी पनपी है जिसे नास्तिकवाद के समकक्ष ही कह सकते हैं। वह है—छुट-पुट कर्मकाण्डों के आधार पर पाप दंड से छुटकारा मिल जाने का समर्थन। इन दिनों सम्प्रदाय वादियों ने अपने अपने मत-सम्प्रदाय के अनुयायी बनाने और बढ़ाने के लिए एक सस्ता नुस्खा ढूंढ़ निकाला है कि उनके मत के अनुसार बताये पूजा विधान, मन्त्र या क्रियाकृत्य की अत्यन्त सरल विधि पूरी कर लेने से जीवन भर के समस्त पापों के दण्ड से छुटकारा मिल जाता है। यह प्रलोभन इसलिए दिया गया प्रतीत होता है कि पाप दण्ड की कष्टसाध्य प्रक्रिया से सहज ही छुटकारा मिल जाने का भारी लाभ देखकर लोग उनके सम्प्रदाय की रीति-नीति अपना लेंगे। यदि बात इतनी भर होती तो भी क्षम्य थी पर इस मान्यता में एक अत्यन्त भयानक प्रतिक्रिया भी जुड़ी है जिसके कारण वह प्रलोभन व्यक्तिगत चरित्र और समाजगत सुव्यवस्था पर घातक प्रभाव डालता है। मनुष्य पापदण्ड से निर्भय हो जाता है। दुष्कर्म करने का उसे प्रोत्साहन साहस मिलता है। जब अनीति अपना कर भरपूर लाभ उठाया जा सकता है और उनके दण्ड से छुटपुट कर्म-काण्ड का आश्रय ही बचा सकता है तो फिर कोई क्यों अनीति आचरण के लाभ को छोड़ना चाहेगा?
नास्तिकवाद और इस पाप दण्ड से बचाने वाले अनास्तिकवाद का निष्कर्ष एक ही है। नास्तिक इसलिए पाप से निश्चित होता है कि सरकार और समाज को चकमा देने के बाद ईश्वर, परलोक कर्मफल आदि का अतिरिक्त झंझट नहीं रह जाता। ठीक इसी निर्णय पर विकृति चिन्तन से भरा प्रचलित ईश्वरवाद भी पहुंचाता है। इस प्रकार वे बाहर से एक-दूसरे के प्रतिकूल दीखते हुए भी निष्कर्ष एक ही निकालते हैं। पापाचरण के लिए दोनों ही समान रूप से पथ प्रशस्त करते हैं।
एक और प्रश्न पर भी वे दोनों एक मत हैं। पुण्य परमार्थ की आवश्यकता नास्तिकवाद नहीं मानना—क्योंकि इससे धन और समय बर्बाद हो जाता है, जब पुण्य प्रतिफल ही नहीं मिलने वाला है तो प्रत्यक्ष घाटा देने वाले परोपकार जैसे कार्यों को क्यों किया जाय? प्रचलित विकृत अध्यात्मवाद भी यही सिखाता है जब छुट-पुट कर्म-काण्डों के नाम जप आदि से ही अक्षय पुण्य मिल जाता है और स्वर्ग मुक्ति तक का द्वार खुल जाता है तो खर्चीले एवं कष्टसाध्य परमार्थ प्रयोजनों को अपनाने से क्या लाभ? प्रकारान्तर से सेवा सत्कर्मों की निरर्थकता सिद्ध करने में भी यह दोनों ही दर्शन एक मत हैं।
नास्तिकवाद के दुष्परिणामों पर समाज के मूर्धन्य लोग विचार करते रहे हैं और उसे अपनाने पर उत्पन्न होने वाले चरित्र संकट की विभीषिका समझाते रहे हैं। पर न जाने दूसरे उस प्रच्छन्न नास्तिकवाद की ओर विचारशील लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता जो छुट-पुट कर्मकांडों का अतिशयोक्तिपूर्ण महात्म्य बताकर पापदण्ड से निर्भय रहने और निरर्थकता सिद्ध करने में प्रकारान्तर से नास्तिकवाद का सहोदर भाई भी सिद्ध होता है। धर्म, अध्यात्म और ईश्वरवाद के मूल प्रयोजन की यह पृच्छन्न नास्तिकवाद जड़ ही काट रहा है इसलिए उसे भी निरस्त किये जाने की आवश्यकता है।
ईश्वर विश्वास क्यों आवश्यक
ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास, कोरी भावुकता या अविकसित मनोभूमि वाले लोगों को पुरस्कार और दंड के प्रलोभन भय से नीति-मार्ग पर अग्रसर तथा अनीति से विरत करने भर का उपाय नहीं है। नहीं यह काल्पनिक उड़ान ही है। ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण सृष्टि के कण-कण में क्षण-प्रतिक्षण देखा जा सकता है उसके अस्तित्व को स्वीकार भर करने से काम नहीं चलता। सूर्य है और प्रतिदिन निकलता है लेकिन उसके प्रकाश में न बैठा जाय, अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां सभी बंद रखे जायें तो यह मानने भर से सूर्य की उपस्थिति का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
आस्तिकता का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व को मानने न मानने तक ही सीमित नहीं है। उसका असली अर्थ तो ईश्वर की विधि व्यवस्था, नियम मर्यादा और नीति सदाचार की प्रेरणाओं को हृदयंगम करना तथा आचार व्यवहार में उतारना है इस स्थिति को ही ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास कहा जा सकता है।
मनुष्य और समाज पर नैतिक नियमों-मर्यादाओं का अंकुश बनाये रखने के लिए ईश्वर विश्वास ही समर्थ है।
ईश्वर विश्वास की इसलिए भी आवश्यकता है कि उसके सहारे हम जीवन का स्वरूप, लक्ष एवं उपयोग समझने में समर्थ होते हैं। यदि ईश्वरीय विधान को अमान्य ठहरा दिया जाय तो फिर मत्स्यन्याय का ही बोलबाला रहेगा। आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव में बाह्य नियन्त्रण मनुष्य जैसे चतुर प्राणी के लिए कुछ बहुत अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। नियंत्रण के अभाव में सब कुछ अनिश्चित और अविश्वस्त बन जायगा। ऐसी दशा में, हमें आदिमकाल में, वन्य स्थिति में वापिस लौटना पड़ेगा और शरीर निर्वाह करते रहने के लिए पेट प्रजनन एवं सुरक्षा जैसे पशु प्रयत्नों तक सीमित रहना पड़ेगा। ईश्वर विश्वास ने आत्म-नियन्त्रण का पथ-प्रशस्त किया है और उसी आधार पर मानवी, सभ्यता की आचार संहिता का, स्नेह, सहयोग एवं विकास परिष्कार का पथ-प्रशस्त किया है। यदि मान्यता क्षेत्र से ईश्वरीय सत्ता को हटा दिया जाय तो फिर संयम और उदारता जैसी मानवी विशेषताओं को बनाये रहने का कोई दार्शनिक आधार शेष न रह जायगा। तब चिन्तन क्षेत्र में जो उच्छृंखलता प्रवेश करेंगी उसके दुष्परिणाम वैसे ही प्रस्तुत होंगे जैसे कि पुराणकाल की कथा गाथाओं में असुरों के नृशंस क्रिया-कलाप का वर्णन पढ़ने-सुनने को मिलता है।
ईश्वर अन्ध विश्वास नहीं एक तथ्य है। विश्व की व्यवस्था सुनियन्त्रित है, सूर्य, चन्द्र, ग्रह नक्षत्र आदि सभी का उदय-अस्त क्रम अपने ढर्रे पर ठीक तरह चल रहा है, प्रत्येक प्राणी अपने ही जैसी सन्तान उत्पन्न करता है और हर बीज अपनी ही जाति का पौधा उत्पन्न करता है। अणु-परमाणुओं से लेकर समुद्र, पर्वतों तक की उत्पादन वृद्धि एवं मरण का क्रिया-कलाप अपने ढंग से ठीक प्रकार चल रहा है। शरीर और मस्तिष्क की संरचना और कार्यशैली देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतनी सुव्यवस्थित कार्यपद्धति बिना किसी चेतना शक्ति के अनायास ही नहीं चल सकती। उस नियन्ता का अस्तित्व जड़ और चेतन के दोनों क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष की दोनों कसौटियों पर पूर्णतया खरा सिद्ध होता है। वह समय चला गया जब अधकचरे विज्ञान के नाम पर संसार क्रम को स्वसंचालित और प्राणी को चलता-फिरता पौधा मात्र ठहराया गया था। अब पदार्थ विज्ञान और चेतन विज्ञान में इतनी प्रौढ़ता आ गई है कि वे नियामक चेतना शक्ति के अस्तित्व को बिना किसी आना-कानी के स्वीकार कर सकें। कर्मफल की व्यवस्था भी उसी नियन्त्रण के अन्तर्गत आती है। समाज और शासन द्वारा दण्ड, पुरस्कार की व्यवस्था है। ईश्वरीय न्याय में भी सत्कर्मों और दुष्कर्मों के लिए समुचित पुरस्कार और दण्ड का विधान है। देर तो मुकदमे होने में भी लगती है और बीज बोने के बाद फसल काटने में भी। इस व्यवस्था को स्थूल बुद्धि समझ नहीं पाती। सत्कर्मों का फल तत्काल न मिलने पर लोग अधीर होने लगते हैं और दुष्कर्मों का तात्कालिक लाभ देखकर उनके लिए आतुरता प्रकट करते हैं। इन भूलभुलैयों में भटका व्यक्ति अपना और समाज का भविष्य अन्धकारमय बनाता है और वर्तमान को अवांछनीयताओं से भर देता है। इस गड़बड़ी की रोकथाम में ईश्वर विश्वास से भारी सहायता मिलती है और व्यक्तिगत चरित्र-निष्ठा एवं समाजगत सुव्यवस्था का आधार सुदृढ़ बना रहता है। इन्हीं सब दूरगामी परिणामों को देखते हुए तत्वज्ञानियों ने ईश्वर विश्वास को दृढ़तापूर्वक अपनाये रहने के लिए जन साधारण को विशेष रूप से प्रेरणा दी है। वह आधार दुर्बल न होने पाये, हर रोज स्मृतिपटल पर जमा रहे इसलिए साधना, उपासना के धर्मकृत्यों का सुविस्तृत विधि-विधान विनिर्मित किया है। इन्हें अपनाकर मनुष्य दिव्यसत्ता को अपने भीतर बाहर विद्यमान देखता है और कुमार्ग से विरत रहकर सन्मार्ग पर चलने का अधिक उत्साह के साथ प्रयत्न करता है। ईश्वर विश्वास के फलस्वरूप पशु प्रवृत्तियों के नियन्त्रण में भारी सहायता मिलती है और व्यक्ति तथा समाज का स्तर सन्तुलित बनाये रहने का प्रयोजन बहुत अंशों तक पूरा होता है। नास्तिकता अपनाकर विश्व-शान्ति का—मानवी उत्कृष्टता का आधार ही डगमगाने लगेगा, इसलिए तत्वदर्शियों ने आध्यात्मिक अनास्था नास्तिकता की कठोर शब्दों में भर्त्सना की है।
जीवन-दर्शन को ईश्वर विश्वास से उच्चस्तरीय प्रेरणा मिलती है। संसार के सभी प्राणी ईश्वर पुत्र हैं। कोई न्यायप्रिय, निष्पक्ष पिता अपनी सभी सन्तानों को लगभग समान स्नेह और समान अनुदान देने का प्रयत्न करता है। ईश्वर ने अन्य प्राणियों को मात्र शरीर निर्वाह जितनी बुद्धि और सुविधा दी तथा मनुष्य को बोलने, सोचने, पढ़ने, कमाने, बनाने आदि की अनेकों विभूतियां दी हैं। अन्य प्राणियों की और मनुष्यों की स्थिति की तुलना करने पर जमीन-आसमान जैसा अन्तर दिखाई पड़ता है। इसमें पक्षपात और अनीति का आक्षेप ईश्वर पर लगता है। जब सामान्य प्राणी अपनी सन्तान को समान स्नेह, सहयोग देते हैं तो फिर ईश्वर ने इतना अन्तर किसलिए रखा? एक को इतना ऊंचा और दूसरे को इतना नीचा कैसे रखा? इस विभेद को समझने में प्रत्येक विवेक सम्पन्न व्यक्ति को भारी उलझन का सामना करना पड़ता है। तत्वदर्शी विवेक बुद्धि इस विभेद के अन्तर का कारण भली प्रकार स्पष्ट कर देती है। मनुष्य को अपने वरिष्ठ सहकारी ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सृजा गया है। उसके कन्धों पर सृष्टि को अधिक सुन्दर, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके लिए उसे विशिष्ठ साधन उसी विशिष्ठ प्रयोजन के लिए अमानत के रूप में दिये गये हैं। मिनिस्टरों को सामान्य कर्मचारियों की तुलना में सरकार अधिक सुविधा साधन इसलिए देती है कि उनकी सहायता से वे अपने विशिष्ठ उत्तरदायित्वों का निर्वाह सुविधापूर्वक कर सकें। यह सुविधाएं उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरन् जन-सेवा के लिए दी जाती हैं। बैंक के खजानची के हाथ में बहुत-सा पैसा रहता है यह उसके निजी उपभोग के लिए बैंक प्रयोजन के लिए अमानत रूप में रहता है। निजी प्रयोजन के लिए तो क्या मिनिस्टर, क्या खजानची सभी को सीमित सुविधा मिलती हैं। अत्यधिक साधन जो उनके हाथ में रहते हैं उन्हें वे निर्दिष्ट कार्यों में ही खर्च कर सकते हैं। निजी कार्यों में उपभोग करने लगें तो यह दण्डनीय अपराध होगा।
ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास सामान्य प्राणियों को उपलब्ध शरीर निर्वाह भर के साधनों से अतिरिक्त जो कुछ भी श्रम, समय, बुद्धि, वैभव, धन, प्रभाव, प्रतिभा आदि की विभूतियां हैं, वह सभी लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए मिली हुई सार्वजनिक सम्पत्ति है। शरीर रक्षा एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए औसत नागरिक-स्तर का निर्वाह कर लेने के अतिरिक्त मनुष्य के पास जो कुछ बचता है उसकी एक-एक बूंद उसे लोक-कल्याण के लिए नियोजित करनी चाहिए। इसी में ईश्वरीय अनुदान और मानवी गरिमा की सार्थकता है। प्रत्येक आस्तिक को सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन की गरिमा, उपयोगिता और जिम्मेदारी समझनी चाहिए तथा उसी के अनुरूप अपने चिन्तन तथा कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। अपनी विशेषताओं का उपयोग इसी महान प्रयोजन के लिए करना चाहिए।
जीवन-दर्शन की यह उत्कृष्ट प्रेरणा ईश्वर विश्वास के आधार पर ही मिलती है। जीवन क्या है, क्यों है, उसका लक्ष्य एवं उपयोग क्या है? इन प्रश्नों का समाधान मात्र आस्तिकता के साथ जुड़ी हुई दिव्य दूरदर्शिता के आधार पर ही मिलता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित मनुष्य संकीर्ण स्वार्थपरता से—वासना, तृष्णा के भव-बन्धनों से छुटकारा पाकर आत्म-निर्माण की ओर—आत्म विस्तार की ओर—आत्म-विकास की ओर अग्रसर होता है और ऐतिहासिक महामानवों जैसी देव भूमिका अपनाने के लिए अग्रसर होता है। व्यक्ति और समाज के कल्याण के महान् आधार खड़े करने वाली यह एक बहुत बड़ी दार्शनिक उपलब्धि है। यदि आस्तिकता का यही स्वरूप समझा जा सके और जीवन-दर्शन के साथ उसे ठीक प्रकार जोड़ा जा सके तो निश्चय ही मनुष्य में देवत्व का उदय और इसी धरती पर स्वर्ग का अवतरण सम्भव हो सकता है। यही तो ईश्वर द्वारा मनुष्य सृजन का एकमात्र उद्देश्य है।
सृष्टि के सभी प्राणी एक पिता के पुत्र होने के नाते सहोदर भाई हैं और वे परस्पर एक-दूसरे का स्नेह, सहयोग पाने के अधिकारी हैं। आस्तिकता यही मान्यता अपनाने के लिए प्रत्येक विचारशील को प्रेरणा देती है। इसका अनुसरण करके प्राणिमात्र के बीच आत्मीयता की भावना विकसित हो सकती है और उसके आधार पर एक-दूसरे के दुःख-दर्द को अपना समझने एवं उदार व्यवहार करने की आकांक्षा प्रबल हो सकती है। विश्व-कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार की भावनात्मक स्थापनाएं अतीव श्रेयस्कर परिणाम प्रस्तुत कर सकती हैं। कहना न होगा कि यह दृष्टिकोण हर दृष्टि से—हर क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य की भूमिका प्रस्तुत कर सकने वाला सिद्ध हो सकता है। ईश्वर विश्वास के कल्पवृक्ष पर तीन फल लगते बताये गये हैं—(1) सिद्धि (2) स्वर्ग (3) मुक्ति। सिद्धि का अर्थ है प्रतिभावान परिष्कृत व्यक्तित्व और उसके आधार पर बन पड़ने वाले प्रबल पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया अनेकानेक भौतिक सफलताओं के रूप में प्राप्त होना। स्पष्ट है कि चिरस्थायी और प्रशंसनीय सफलताएं गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता के फलस्वरूप ही उपलब्ध होती हैं। मनुष्य को दुष्प्रवृत्तियों से विरत करने और सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उत्कृष्ट चिन्तन और आदर्श कर्तृत्व अपनाना पड़ता है। यह सभी आधार आस्तिकतावादी दर्शन में कूट-कूटकर भरे हैं। आज का विकृत अध्यात्म-दर्शन तो मनुष्य को उलटे भ्रम-जंजालों में फंसाकर सामान्य व्यक्तियों से भी गई-गुजरी स्थिति में धकेलता है, पर यदि उसका यथार्थ स्वरूप विदित हो तो उसे अपनाने का साहस बन पड़े तो निश्चित रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। जहां यह सफलता मिली वहां अन्य सफलतायें हाथ बांधकर सामने खड़ी दिखाई पड़ेंगीं। महामानवों द्वारा प्रस्तुत किये गये चमत्कारी क्रिया-कलाप इसी तथ्य की साक्षी देते हैं। इसी को सिद्धि करते हैं। अध्यात्मवादी आस्तिक व्यक्ति चमत्कारी सिद्धियों से भरे-पूरे होते हैं। इस मान्यता को उपरोक्त आधार पर अक्षरशः सही ठहराया जा सकता है। किन्तु यदि सिद्धि का मतलब बाजीगरी जैसी अचम्भे में डालने वाली करामातें समझा जाय तो यही कहा जायगा कि वैसा दिखाने वाले धूर्त और देखने के लिए लालायित व्यक्ति मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।
आस्तिकता के कल्पवृक्ष पर लगने वाला दूसरा फल है—स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ है—परिष्कृत गुणग्राही विधायक दृष्टिकोण। परिष्कृत दृष्टिकोण होने पर अभावग्रस्त दरिद्र मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मनुष्य जीवन अपने आप में इतना पूर्ण है कि उस सम्पत्ति को संसार की समस्त एकत्रित सम्पदा की तुलना में भी अधिक भारी माना जा सकता है। शरीर यात्रा के अनिवार्य साधन प्रायः हर किसी को मिले होते हैं, अभाव तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकने के कारण ही प्रतीत होता है। अभावों की, कठिनाइयों की, विरोधियों की लिस्ट फाड़ फेंकी जाय और उपलब्धियों, सुविधाओं, सहयोगियों की सूची नये सिरे से बनाई जाय तो प्रतीत होगा कि कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दरिद्र चला गया, उसके स्थान पर वैभव आ विराजा। छिद्रान्वेषण की आदत हटाकर गुण ग्राहकता अपनाई जाय तो प्रतीत होगा कि इस संसार में ईश्वरीय उद्यान की—नन्दन वन की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। स्वर्ग इसी विधायक दृष्टिकोण का नाम है—जिसे अपनाकर अपनी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की देव सम्पदा को हर घड़ी प्रसन्न रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। स्वर्ग और नरक कोई क्षेत्र नहीं वरन् लोक हैं। लोक का अर्थ है दृष्टिकोण। निकृष्ट चिन्तन की प्रतिक्रिया नारकीय दुःख दारिद्रय से भरी हुई होती है और उत्कृष्टता भरी विचारणाओं का प्रतिफल स्वर्ग जैसी सुख-शान्ति प्रस्तुत करता रहता है। ईश्वर विश्वास की राह पर चलता हुआ मनुष्य स्वर्गीय वातावरण प्रस्तुत करता है, उसमें स्वयं रहते हुए आनन्द अनुभव करता है और समीपवर्ती क्षेत्र को उसी प्रकाश से दीप्तिवान बनाता है।
आस्तिकता का तीसरा प्रतिफल है—मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है—अवांछनीय भव-बन्धनों से छूटना। अपनी दुष्प्रवृत्ति, मूढ़ मान्यताएं एवं विकृत आकांक्षाएं ही वस्तुतः सर्वनाश करने वाली पिशाचिनी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, चिंता, भय, दैन्य जैसे मनोविकार ही व्यक्तित्व को गिराते, गलाते, जलाते हैं। आधि और व्याधि इन्हीं के आमन्त्रण पर आक्रमण करती हैं। आस्तिकता इन्हीं दुर्बलताओं से जूझने की प्रेरणा भरती है। सारा साधना शास्त्र इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ने, खदेड़ने की पृष्ठभूमि विनिर्मित करने के लिए खड़ा किया गया है। इनसे छुटकारा पान पर देवत्व द्रुतगति से उभरता है और अपनी स्वतन्त्र सत्ता का उल्लास भरा अनुभव होता है।
मनुष्य कितने ही दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों, पक्षपातों, प्रचलनों, अनुकरणों से घिरा बंधा कंटकाकीर्ण राह पर घिसटता रहता है। स्वतंत्र चिन्तन की विवेक दृष्टि उसे कदाचित ही मिल पाती है। यदि वह मिली होती तो निश्चय ही औचित्य को प्रश्रय दिया गया होता और तथाकथित मित्र, परिचित क्या कहते हैं? इसकी पूर्णतया उपेक्षा करके विवेक के प्रकाश में कदम बढ़ाने का साहस संजोया होता। महामानव इसी सत्साहस के बल पर स्वयं धन्य बने हैं और अपने युग को—क्षेत्र को धन्य बनाया है। जीवन-मुक्त पुरुष अवांछनीय चिन्तन से मुक्त होते हैं और आत्मिक स्वतन्त्रता का आनन्द लेते हैं। स्पष्ट है कि ईश्वर भक्तों को संयमी, स्वार्थपरता से रहित, लोकोपयोगी ब्राह्मण और साधु स्तर का जीवन जीना पड़ता है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ईश्वर विश्वास अपनाकर हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं और उसे पाकर रहते हैं।