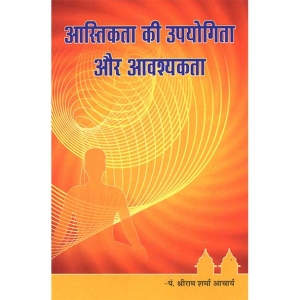आस्तिकता की उपयोगिता और आवश्यकता 
आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध
Read Scan Versionजीव क्या है? चेतना के विशाल सागर की एक छोटी सी बूंद अथवा लहर। हर शरीर में थोड़ा आकाश भरा होता है, उसका विस्तार सीमित है उसे नापा और जाना जा सकता है, पर वह अलग दीखते हुए भी ब्रह्माण्ड व्यापी आकाश का ही एक घटक है। उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं। जब तक वह काया कलेश्वर में घिरा है तभी तक सीमित है, काया के नष्ट होते ही वह विशाल आकाश में जा मिलता है। फेफड़ों में भरी सांस सीमित है। पानी का बबूला स्वतंत्र है, फिर भी इनके सीमा बन्धन अवास्तविक है। फेफड़े में भरी वायु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ब्रह्माण्ड व्यापी वायु ही परिस्थितिवश फेफड़ों की छोटी परिधि में कैद है। बन्धन न रहने पर वह व्यापक वायुतत्त्व से पृथक दृष्टिगोचर न होगी। पानी का बबूला हलचलें तो स्वतंत्र करता दीखता है पर हवा और पानी का छोटा-सा संयोग जिस क्षण भी झीना पड़ता है पानी पानी में और हवा हवा में जा मिलती है। बबूले का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
जीव अर्थात व्यापक ईश्वरीय सत्ता का परिस्थितिवश स्वतंत्र दिखाई पड़ने वाला एक छोटा और अस्थायी घटक। चेतना का एक असीम समुद्र सर्वत्र लहलहा रहा है। हम सब उसी में जन्मने, मरने और जीवित रहने वाले जल जन्तु हैं। यह उपमा अधूरी लगती हो तो सागर और उसकी लहरों का उदाहरण ठीक समझा जा सकता है। हर लहर पर एक स्वतंत्र सूर्य चमकता देखा जा सकता है, पर उतने सूर्य है नहीं। यह दृश्य की विचित्रता है। वस्तुतः एक ही सूर्य के पृथक प्रतिबिम्ब भर चमकते हैं।
जीव और ईश्वर के संबंध की यथार्थता को समक्ष लेने पर कई बातें उभर का आती हैं एक तो यह है कि अंश में अंशी के समस्त गुण होने चाहिए दूसरे यह कि पृथकता के पर्दे में पीछे से झांकती हुई एकता का दर्शन किया जाना चाहिए। और भी कई तथ्य हैं जो सत्य के निकट तक पहुंचाते हैं पर अभी हमें इन दो पर ही विचार कर लेना उचित होगा।
आग की छोटी चिनगारी में वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो विशाल कार्य भट्टी में पाई जाती हैं। चिनगारी में गर्मी भी है और रोशनी भी। यदि अवसर मिले तो उपयुक्त ईंधन पाकर उसकी लघुता सुविस्तृत हो सकती है। आकार को लघुता विशालता तो यथार्थ है पर संभावना-तात्त्विकता एवं एकता में कोई अन्तर नहीं। जीवात्मा उन्हीं विशेषताओं और संभावनाओं से भरा पूरा है जो परमात्मा में विद्यमान है। इतना होते हुए भी चिनगारी अपने छोटे पन के कारण दुर्बल और अशक्त दिखाई पड़ती है। कई बार तो वह दुर्गन्ध युक्त ईंधन के साथ रहने पर हेय और घृणित भी प्रतीत होती है। चन्दन की लकड़ी में और मल के ढेर में जलने वाली अग्नियों में से एक आनन्द दायक होती है और सुगन्ध कहलाती है दूसरी कष्ट कारक दुर्गन्ध के रूप में तिरस्कृत होती है। यद्यपि मूलतः एक ही अग्नि तत्व इन दोनों स्थानों में काम कर रहा होता है।
आत्मा की महिमा और गरिमा को समझा जा सके तो उसे उसके स्तर के अनुरूप स्थिति में रखने की इच्छा होगी। इसके लिए जगी अभिलाषा और विकसित हुई स्थिति आत्म गौरव कहलाती है। गौरवान्वित को सन्तोष मिलता है और आनन्द भी। तिरस्कृत को हीनता अनुभव होती है और लज्जित एवं दुखी रहना पड़ता है। आत्म बोध जब तक न हो तब तक भेड़ों के झुण्ड में पले सिंह शावक की तरह हेय स्थिति में नर पशु की तरह रहना पड़ता है पर जिस क्षण अपने अस्तित्व की यथार्थता एवं गरिमा का बोध होता है उसी समय में वह आतुरता उत्पन्न होती है कि लज्जास्पद स्थिति से उबरना ही चाहिए। गौरवान्वित होकर ही रहना चाहिए। हेय और हीन बनकर रहना जब धिक्कार के योग्य लगता है तो भीतर से एक विशेष तड़पन और तिलमिलाहट उठती है। तत्व ज्ञानियों ने इसी स्थिति को ईश्वर भक्ति कहा है। हेय स्तर अर्थात् भव बन्धन। उत्कृष्ट स्वाभाविकता अर्थात ईश्वर मिलन।
ब्रह्म विद्या में आत्म बोध को प्रथम स्थान दिया गया है और अपने आपे की वास्तविकता समझाने के लिए कई सूत्र संकेत दिये गये हैं अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानब्रह्म, शिवोऽहम्, सच्चिदानंदोऽहम्—सोऽहम्—तत्वमसि आदि सूत्रों में ईश्वर और आत्मा की एकता का प्रतिपादन है। अंश और अंशी की स्थिति का उद्बोधन है। जीवन चेतना को ब्रह्म चेतना का छोटा संस्करण माना गया है और कहा गया है कि उसमें सत्, चित्, आनन्द की सत्यं शिवं सुन्दरम् की समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं।
संकट प्रसुप्त स्थिति का है। सोया हुआ मनुष्य अर्धमृतक स्थिति में पड़ा रहता है। उस स्थिति में उसे गन्दगी, दुर्गन्ध, अपमान, दुर्गति का बोध नहीं होता। कुछ भी भला बुरा होता रहे गहरी नींद में कुछ सूझता ही नहीं ठीक आत्म बोध से रहित स्थिति में जीव की असीम दुर्गति रहती है। खुमारी यह विदित ही नहीं होने देती कि उसकी कैसी दुर्गति हो रही है। इस खुमारी के कारण उत्पन्न हुई अर्ध मूर्छित स्थिति को ‘माया’ कहते हैं। माया को ही जीव की दयनीय दुर्गति का कारण बताया गया है।
माया ग्रसित स्थिति में जीव अपने को आत्मा न मानकर शरीर अनुभव करने लगता है। और उसी के लाभ हानि को अपना मानने लगता है। इसकी इच्छा आकांक्षा अभिरुचि इन्हीं बातों में सीमाबद्ध हो जाती है जो शरीर और मन को प्रिय है। अपने स्वरूप को भूला हुआ आत्मा अपने लक्ष्य, एवं हित को भी भूल जाता है और मात्र उतना ही सोचता है जितना शरीर को रुचिकर लगे। यह विचित्र स्थिति है कि कोई अपने वाहन, उपकरण, वस्त्र घर आदि को सुसज्जित रखने के लिए तो समय, बुद्धि और धन को खर्च करता रहे किन्तु अपनी भूख प्यास का, आरोग्य आजीविका का कुछ भी विचार न करे। शरीर और मन जीवन रथ के दो पहिये हैं इन्हें दो घोड़े दो सेवक भी कहा जा सकता है। इनके सहारे जीवन यात्रा सुविधा पूर्वक सम्पन्न हो सके इस लिए परम पिता ने अपने राजकुमार के लिए इन बहुमूल्य साधनों की व्यवस्था की है। इन्हें संभालकर रखा जाना चाहिए और सदुपयोग किया जाना चाहिए यह बुद्धिमत्ता पूर्ण है। किन्तु जब जीव अपना लक्ष्य भूलकर मात्र इन दो वाहनों की साज सज्जा में लगे रहने के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं तो इस स्थिति को माया मूढ़ता कहते हैं।
जीव की उत्कृष्ट और असीम संभावनाओं से भरी पूरी स्थिति को दीन दयनीय स्थिति से घिरा देखा जाय तो यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं मानी जानी चाहिए, वरन् माया मूढ़ता का अभिशाप समझा जाना चाहिए। बन्धनों की जकड़न शरीर और मन के लिए इतनी कष्टकारक होती है इसे कोई भी भुक्तभोगी समझ सकता है। किसी के हाथ पैर कसकर मुंह से पट्टी बांधकर अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाय तो उसे कितनी शारीरिक पीड़ा और मानसिक व्यथा होगी इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। ईश्वर के अंश जीव की दुर्गति का कारण यही माया बन्धन है। इन्हीं को काटने के लिए जो प्रबल पुरुषार्थ किया जाता है उसे साधना एवं उपासना कहते हैं।
ईश्वर भक्ति का अत्यधिक माहात्म्य बताया गया है। उसके असंख्य भौतिक एवं आत्मिक लाभ गिनाये गये हैं। वह प्रतिपादन सर्वथा सही है। भक्ति का प्रयोजन—अपना मूल स्वरूप समझना और मायाजन्य दुर्गति से छुटकारा प्राप्त करना है। आत्म बोध को इसी परिवर्तन का केन्द्र बिन्दु माना गया है। इसे आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर दर्शन भी कहते हैं। बन्धन मुक्ति, जीवन मुक्ति, नव जागृति, प्रकाश प्राप्ति आदि शब्दों में इसी स्थिति की चर्चा की गई है। इस उपलब्धि को परम पुरुषार्थ की परम सफलता कहा गया है। इस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को जो दिव्य संतुष्टि एवं प्रसन्नता होती है उसे ब्रह्मानन्द परमानन्द आदि के नाम से जाना जाता है। इसी को जीवन लक्ष्य की पूर्ति कहते हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्न करने पड़ते हैं उन्हें योग और तप के नाम से पुकारते हैं।
बिजली घर से सम्बन्धित रहने पर बल्ब जलते और पंखे चलते हैं। कनेक्शन कट जाने पर अच्छे खासे विद्युत उपकरण भी गति हीन बने पड़े रहते हैं। ईश्वर और आत्मा के बीच सघन आदान प्रदान की श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिये भक्ति भावना की आवश्यकता पड़ती है। चेतना का स्वरूप भावनात्मक है। उसमें संवेदना भरी रहती है। सह से बड़ी सब से प्रखर भावना प्रेम है। इसी को भक्ति कहते हैं। इसी के साथ-साथ दया करुण, उदारता, सेवा, सहकारिता, पवित्रता, जैसी अन्य उदात्त भावनाएं सहचरी बन कर चलती है। इन्हें प्रेमरूपी सूर्य की किरणें भी कह सकते हैं। ईश्वर दिव्य संवेदनाओं का केन्द्र है। उसके साथ घनिष्ठता के संबंध जोड़ने के लिए भक्ति भावना के विकास का अभ्यास करना पड़ता है उपासनात्मक अनेकों क्रिया-प्रतिक्रियाएं इसी आत्म विकास का पथ प्रशस्त करती है।
ईश्वर की महिमा अपार है, उसकी सामर्थ्य अनन्त है, उसका कर्तृत्व महान है, जो कुछ महत्वपूर्ण है सभी उसके गर्भ में विद्यमान है, मनुष्य की इच्छा और आवश्यकता को पूरा कर सकने से कहीं अधिक विभूतियां ईश्वरीय सत्ता में विद्यमान हैं पर अपनी पकड़ और पात्रता स्वल्प होने के कारण जो मिलता है वह स्वल्प होता है। स्वल्प से संतोष नहीं होता। अपनी सत्ता लघु है इसलिए उसके उपार्जन भी सीमित रहते है। असीम आकांक्षाओं की तृप्ति असीम के समुद्र में ही मिलने से पूरी होती है। गंगा का उद्भव हिमालय से हुआ है तो भी वह जानती है कि वह स्वयं पाषाण नहीं जल है। पत्थर के टुकड़े पत्थर के ढेर में जमा होने पर गर्व कर सकते हैं पर जल धारा को तो असीम जल राशि में मिल कर ही पूर्णता का आनन्द मिल सकता है। अस्तु गंगा की धारा दौड़ती हुई समुद्र तक पहुंचती है और उसी में विलीन हो जाती है।
जीवात्मा को गंगा की तरह भौतिकता के पाषाण पर्वत से असन्तोष ही बना रहता है। तृप्तिदायक संतोष उसे असीम के अधिष्ठाता ईश्वर के साथ मिलने पर ही हो सकता है। यही है वह आकांक्षा जिसके अतृप्त रहने पर वह हर दिशा में प्यासा फिरता है और निराशा हाथ लगने पर थकान से चूर और खीज से उद्विग्न बना रहता है। मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरन की तरह जीव भी एक छोड़ दूसरा तृप्ति का आधार खोजता है। दूसरे से तीसरे पर और तीसरे से चौथे पर उसकी खोज चलती रहती है। हर प्रयास के बाद नई प्यास की अतृप्ति तब तक चलती रहती है जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। गंगा को समुद्र में मिलने से ही तो शान्ति मिल सकी है।
आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का परम लक्ष्य और परम लाभ है इसी को प्राप्त करने के लिए लम्बा मार्ग पूरा करना पड़ता है। अमीबा से लेकर बन्दर तक—और बन्दर से मनुष्य तक की लम्बी यात्रा इसी प्रयोजन के लिए पूरी करनी पड़ी है कि लघु से महान बनने के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके अनुभव लिए जायें और क्रमशः अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपूर्णता से चलकर पूर्णता तक पहुंचा जाय। इसी क्रीड़ा कल्लोल में जीव को धकेला गया है। प्रायः सभी पशु-पक्षी अपने बच्चों को सुयोग्य एवं समर्थ बनाने के लिए इसी तरह की शिक्षा पद्धति से काम लेते हैं। सम्भवतः ईश्वर ने भी जीव को क्रमशः अधिकाधिक सक्षम बनने की लम्बी यात्रा पर चल पड़ने के लिये विवश किया है। अन्य योनियों में यह यात्रा धीमी गति से चलती है। बच्चा भी तो ठुमक ठुमक कर चलता है। जवान की सामर्थ्य-परीक्षा लम्बी दौड़ और ऊंची कूद जैसे उपक्रमों से परखी जाती है। मनुष्य जीवन जीवात्मा की जवानी है। उससे उसे पूर्णता का लक्ष्य पूरा करने के लिए विशेष अवसर और विशेष साधन मिला है। तत्व ज्ञानी इसीलिए हर विवेकवान को सजग करते हैं कि वह यथार्थता को समझे। जीवन का मूल्यांकन करे और इस दुर्लभ अवसर का जो लाभ उठाया जा सकता है उसकी ओर से आंखें बन्द न किये रहे।
जीवन का स्वरूप उद्देश्य लक्ष्य और उपयोग समझने-समझाने की पुण्य प्रक्रिया को ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है। इसी को चरम ज्ञान कहा गया है। सामान्य व्यक्ति शरीर के इन्द्रिय सुख और मन के अहंकार तोष को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हीं के लिए साधन जुटाने में निरन्तर लगे रहते हैं। वासना और तृष्णा को पूरा करने में ही उनका मनोयोग श्रम और समय निरत रहता है। कृमि कीटकों से लेकर पशु-पक्षियों तक सभी सामान्य जीव पेट और प्रजनन की प्रेरणा से ही अपनी गति विधियां चलाते हैं। मनुष्य की स्थिति विशेष है। उसे ऊंची बात सोचनी चाहिए और यथार्थता को खोजना चाहिए। समझदारी इसी में है और इसी को दूरदर्शिता, विवेकशीलता एवं बुद्धिमत्ता कह सकते हैं।
‘‘नहिं ज्ञानेन सदृश पवित्र मिह विद्यते’’ की गीता उक्ति में इस लोक की—इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सद्ज्ञान को ही कहा है। जिस पैनी दृष्टि से जीवन का स्वरूप एवं लक्ष्य समझा जा सके और उस दुर्लभ अवसर के सदुपयोग की योजना बन सके, ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान उसी को कहते हैं। यह उपलब्ध होने पर जीवनोद्देश्य को पूर्ण कर सकने वाली निश्चित योजना बन जाती है। दृष्टि साफ हो जाती है और मार्ग के सम्बन्ध में सन्देह नहीं रह जाता। इसे प्रकाश की प्राप्ति कहा गया है और सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है शास्त्रों में इस उपलब्धि के कई नाम हैं ऋतम्भरा प्रज्ञा, दिव्य दृष्टि भूमा आदि। इसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री महा मन्त्र में जिस सविता की समीपता का वरेण्य की उपासना का भर्ग की आराधना का देव की अनुभूति का, धी की धारणा का, प्रकाश की प्रेरणा का अनुरोध आग्रह किया गया है वही एक मात्र ईश्वरीय वरदान है। वह मिल सके तो फिर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इतना मिल जाने के बाद तो उस थोड़े से साहस का अभ्यास करना पड़ता है जिसके सहारे पशु प्रवृत्तियों के अभ्यास की आदत छोड़ी जा सके और दिव्य जीवन की रीति नीति का दिनचर्या में समावेश किया जा सके।
ईश्वर के अति निकट होते हुए भी हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। इन विचित्र व्यामोह का निवारण करने के लिए ही ध्यान प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और जो बहुमूल्य रत्न खो गया है उसे गम्भीरता पूर्वक तलाश करना पड़ता है। आश्चर्य यह है कि अति समीप तत्व हमारे लिए अति दूर बन गया है। गले में बंधे हुए कंठे की याद नहीं रहती है उसकी खोज में भारी दौड़ धूप की जा रही है और तो और उस प्राणप्रिय प्रियतम का हम नाम तक भूल गये हैं और रूप तक विस्मृति के गर्त में चला गया है। कैसी है यह विचित्र स्थिति अपनी। उसे उन्मत्त की विक्षिप्त की मनोदशा कहा जा सकता है। भुलक्कड़ तो तरह-तरह के देखे गये हैं पर जो अपने को अपने लक्ष्य को ही भूल बैठे उसके लिए क्या कहा जाय? ऐसी विचित्रता हमें अपने भीतर ही दीख पड़ेगी। न अपना स्वरूप याद आता है और न लक्ष्य की स्मृति शेष रही है। इसी विस्मृति को स्मृति में बदलने के लिए नाम जप और इष्टदेव के ध्यान की प्रक्रिया बनाई गई है।
ईश्वर को उसके स्वरूप एवं क्रिया कलाप को—आदर्श निर्देश को यदि देखना खोजना हो तो वह अपने भीतर ही भली प्रकार दृष्टिगोचर हो सकता है। उसे बाहर देखने का मन हो तो उसका स्वरूप और लीला विलास देखने में भी कुछ कठिनाई नहीं है। अन्तर में झांके तो वह परम प्रभु हंसता मुसकराता और कुछ कहता करता दिखाई पड़ेगा। ऊंचा उठने और आगे बढ़ने की अदम्य आकांक्षा ही किसी के भीतर बनी रहती है—आत्म गौरव हर किसी को अभीष्ट है—सत् और असत् का विवेक सभी में है—श्रेष्ठ आचरणों से आत्म संतोष और निकृष्ट से आत्म विद्रोह का अनुभव हर कोई करता है। यही देवत्व है भावना क्षेत्र में इन्हीं दिव्य संवेदनाओं के रूप में ईश्वरीय चेतना को अपने अन्तःकरण में विराजा हुआ देखा जा सकता है। मानवी आत्मा की मूल प्रवृत्तियां यही हैं। भौतिकतावादी अन्वेषणों ने मानवी चेतना को पशु और पिशाच के रूप में खोजा है। ये उसे भय, आक्रमण, स्वार्थ से प्रेरित पीड़ित मानते हैं और प्रकारान्तर से मत्स्य न्याय एवं सर्व भक्षी उपभोग का समर्थन करते हैं। उन्होंने तो जीवन को रासायनिक उत्पादन माना है और पुनर्जन्म, परलोक, कर्म फल, जीव सत्ता एवं परमात्मा के अस्तित्व तक से इंकार किया है। इस समय उस विवाद में नहीं उलझा जा सकता केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यदि यह प्रतिपादन सही रहे होते तो अब तक न्याय, नीति, धर्म, सदाचार एवं मानवी मर्यादाएं कब की समाप्त हो गई होतीं और बुद्धिबल का पैशाचिक प्रयोग करके एक दूसरे का रक्त पान करते हुए मनुष्य कब के मर खप कर समाप्त हो गये होते। तब इस संसार में सद्भावना और आदर्शवादिता नाम की कोई परम्परा शेष नहीं रही होती। यदि अब तक इन तथ्यों का पता न रहा होगा और भौतिकवादी प्रतिपादनों ने इन रहस्यों का उद्घाटन किया होगा तो निश्चय ही अगले दिनों वही मान्यता सर्वत्र स्वीकार्य होगी। यदि वैसा हुआ तो इतनी भविष्यवाणी निश्चित रूप से की जा सकती है कि बुद्धिहीन पशु तो आदर्श विहीन रहकर भी निर्वाह करते रहेंगे पर बुद्धिमान मनुष्य अमर्यादित वासना और अनियन्त्रित तृष्णा को अपना कर पिशाच कृत्यों पर उतरेगा तो राजदण्ड व समाज दंड भी उसे रोक न सकेंगे और स्वच्छन्दतावाद को चिता में कूद कर मानव जाति को सामूहिक आत्म हत्या के लिए विवश होना पड़ेगा।
हमारा विश्वास है कि न तो वे मान्यताएं सही हैं और न उन्हें मानवी विवेक कभी स्वीकार करेगा आत्मा की उत्कृष्टता अक्षुण्ण बनी रहेगी और वह क्रमिक विकास के पथ पर चलते हुए अधिकाधिक समुन्नत परिष्कृत होती चलेगी। जैसे जैसे हम अध्यात्म की यथार्थता और महत्ता को समझेंगे वैसे वैसे उसे अधिक उत्साह पूर्वक अपनाने और अधिक श्रद्धा पूर्वक हृदयंगम करने के लिए उत्साह प्रकट करेंगे। साहस पूर्वक उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करेंगे।
हां तो कहा यह जा रहा था कि अपने भीतर ईश्वर की झांकी उत्कृष्टतावादी और अदम्य सत्प्रेरणाओं के रूप में की जा सकती है। ऊंचा उठने, आगे बढ़ने, गौरवास्पद बनने और आत्म-सन्तोष पाने की आकांक्षा केवल दिव्य जीवन क्रम अपनाकर ही पूरी की जा सकती है। औचित्य अपना कर एक सीमा तक भौतिक उन्नति भी हो सकती है और उसका सदुपयोग भी बन पड़ सकता है पर यदि आदर्श विहीन संग्रह, उपभोग और आतंक की गति अपनाई गई तो आत्मिक आकांक्षाओं में से एक भी पूरी न हो सकेगी। कुछ पाया भी तो वह उतना महंगा पड़ेगा कि बाह्य अवरोध एवं आन्तरिक विद्रोह उसे नीरस एवं भारभूत बनाकर रख देंगे। अन्तःकरण के मर्मस्थल से जिस महानता की प्राप्ति के लिए हूक उठती रहती है उसे उत्कृष्ट आदर्श वादिता अपना कर ही पूरा किया जा सकता है। इसी प्रेरणा को ईश्वरीय चेतना दैवी संदेश आत्मा की पुकार एवं वेदवाणी कहा जा सकता है। जिसकी यह अन्तःप्रेरणा जितनी प्रबल है उसकी आत्मा में ईश्वर की ज्योति उतनी ही अधिक दीप्तिमान देखी जा सकती है।
भगवान के अवतार समय समय पर होते रहे हैं। उनके अवतरण का उद्देश्य एक ही रहा है अधर्म का विनाश और धर्म का संस्थापन। दुष्कृतों का निराकरण और साधुता का परित्राण, इस एक ही प्रयोजन के लिए विभिन्न स्तर के नाम रूप वाले अवतरण हुए हैं। उनके क्रिया कलापों में मित्रता तो रही है पर प्रयोजन एक ही रहा है। जो तथ्य वेद रूप में बाह्य जगत में प्रकट होता रहा है वही अन्तःकरण में भी अवतरित होता हुआ देखा जा सकता है। अपनी भीतरी दुनिया भी कम विस्तृत नहीं है। इसमें भी अनेकों अवांछनीय असुरताएं दुष्प्रवृत्तियों के रूप में अट्टहास करती हुई देखी जा सकती है। ईश्वर का अवतार जिस भी अन्तःकरण में प्रकट होगा वहां उसका दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का कार्य तेजी के साथ सम्पन्न हो रहा होगा। राम अवतार में लंकाकाण्ड का—कृष्ण अवतार में महाभारत का युद्ध प्रसंग सर्व प्रमुख एवं सर्व विदित है। यही अन्तः संघर्ष प्रत्येक ईश्वर भक्त के भीतर चलता है। विकृतियों के प्रति उसका रोष आक्रोश बढ़ता जाता है और क्रियाक्षेत्र में विचार क्षेत्र में जो भी दुष्प्रवृत्तियां जड़ जमाकर बैठ गई है उनके उन्मूलन का प्रयत्न पूर्ण संवेग के साथ चल पड़ता है। भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी का असुर विहीन कर दिया था। रामचन्द्र जी को भी निश्चरहीन करों मही का भुज उठाये प्रण करना पड़ा था। प्रत्येक भक्त अन्तरात्मा में ईश्वर का अवतरण इसी रूप में होता है। भीतर से आरम्भ होकर यह शोधन प्रक्रिया क्रमशः विकसित होती चली जाती है और दीपक जिस प्रकार स्वयं प्रकाशवान बनने के साथ साथ अपने क्षेत्र को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार यदि अवांछनीयताओं का उन्मूलन करने की प्रक्रिया उभरती दीख पड़े तो उस उभार को प्रत्यक्ष ईश्वर दर्शन के रूप में देखा जा सकता है।
ईश्वर के अवतार का दूसरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना—साधुता का उत्कर्ष। यह पूरक प्रक्रिया हुई। अधर्म का उन्मूलन निषेधात्मक—धर्म की स्थापना विधेयात्मक, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नींव खोदने के उपरान्त दीवार चुनी जाती है। खेत जोतने के बाद बीज बोया जाता है। झाड़ियां काटकर समतल खेत बनाये जाते हैं अनीति को हटाकर नीति की स्थापना की जाती है। असुरता का उन्मूलन और देवत्व का अभिवर्धन एक ही प्रयोजन के दो पक्ष हैं। दर्जी कपड़े को काटता भी है और सीता भी है। डॉक्टर आपरेशन के बाद मरहम पट्टी भी करता है। मल विसर्जन जैसे नित्य कर्म करने के बाद भोजन व्यवस्था भी की जाती है। अधर्म का उन्मूलन तभी सार्थक होता है जब उसके साथ साथ धर्म का सृजन भी होता चले। असुरता के विनाश की पूर्णता देवत्व के अभिवर्धन में अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहती है।
किसी में ईश्वर का अवतरण कितने आवेश और आलोक का है उसका निर्धारण इस साधारण आधार पर हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने भीतर और बाहरी क्षेत्र में अवांछनीयताओं के उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्द्धन में कितनी तत्परता के साथ संलग्न है।
दुर्गुणों को हटा देना ही पर्याप्त नहीं, सद्गुणों का बीजारोपण सिंचन एवं अभिवर्धन भी उसी उत्साह के साथ होना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव में समाई हुई दुष्प्रवृत्तियों को हटा देना तो खाई पाट देना भर हुआ। उस स्थान पर नये देव मन्दिर का सृजन करने के साधन भी जुटाये जाने चाहिए। दुर्बुद्धि छोड़ देना एक पक्ष है उतने से तो हानि भर रुकेगी लाभ कमाने के लिए सद्बुद्धि को सक्रिय होना चाहिए। दुहने पात्र के पेंदे में हुए छेद बन्द करने से उसमें भरी वस्तु के फैलने का संकट भर दूर होता है। उस पात्र को दूध से भरने के लिए तो कुछ अन्य आन्तरिक प्रयास करने पड़ेंगे। छेद बन्द कर देने मात्र से कोई व्यक्ति उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता जिसके लिए दूध दुहने वाला पात्र खरीदा गया था।
गुण कर्म, स्वभाव के क्षेत्र में उत्कृष्टता का समावेश करते चलने वाली दिव्य धारा का जब अन्तःकरण में उभार आने लगे तो समझना चाहिए कि ईश्वर का अवतरण हो रहा है। गर्मी की ऋतु आते ही हर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है समझना चाहिए कि व्यक्ति में ईश्वर का अवतरण आदर्शवादी गतिविधियां अपनाने के लिए उत्साह और साहस भरी ऊष्मा उत्पन्न किये बिना रहेगा नहीं। वर्षा ऋतु आती है तो हवा में नमी बढ़ती है और धरती पर हरियाली उगती है। ईश्वर वर्षा ऋतु की तरह है उसकी लहर आती है तो आकाश से सद्भावनाओं के बादल बरसते हैं, कुछ श्रेष्ठ तम कर गुजरने की उमंगें बिजली की तरह कड़कती हैं। जीवन के धरातल पर सत्प्रवृत्तियों की घास अनायास ही उग पड़ती है और जिधर भी नजर उठाई जाय हरितमा नजर आती है। अन्तरंग में सद्गुणों का उभार होता है और बाहर भी इस विश्व उद्यान की शोभा सुन्दरता देखने में आंखें आनन्द अनुभव करती हैं। शीत ऋतु में जिसे भी छुआ जाय ठंडा प्रतीत होता है। अपने भीतर की शांति बढ़ चले और संपर्क क्षेत्र में शान्ति संस्थापन का प्रयास सफल होने लगे तो समझना चाहिए कि यह ईश्वरीय अवतरण का चमत्कार है। वृक्षों के पुराने पत्ते पीले पड़ते और झड़ते हुए शीत ऋतु में देखे जाते हैं। यही हाल ईश्वर भक्ति के प्रभाव से होता है पुरानी वे आदतें, पुरानी वे इच्छाएं, झड़ती गिरती चली जाती हैं जिनके कारण मनुष्य को पेंट और प्रजनन तक सीमा बद्ध व पशु स्तर का जीवन जीना पड़ता है। वसन्त में नये पल्लवों नये पुष्पों से वृक्ष वनस्पतियों को लदा हुआ देखा जाता है। ईश्वर अवतरण का प्रभाव ऐसा उल्लास उत्पन्न करता है जिससे व्यक्तित्व के कण कण देव चेतना का सौन्दर्य खिलता हुआ देखा जा सके। ऋतुओं के प्रभाव से बदलता हुआ वातावरण सहज ही पहचाना जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दिनों अमुक मौसम है। किसी के व्यक्तित्व को—चिन्तन और कर्तृत्व को उत्कृष्टता युक्त देखा जाय तो समझना चाहिए यहां ईश्वरीय अवतरण का पुण्य प्रभाव हो चला।
गंगावतरण की कथा प्रसिद्ध है भागीरथ ने तप किया था और वे उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाये थे। भागीरथी ने विशाल भूखण्ड की प्यास बुझाई और सम्पत्ति उगाई। शिव की जटाओं से भी गंगा के प्रकट होने की चर्चा है। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मलोक है इसी को स्वर्ग कहते हैं। सद्ज्ञान की गंगा का अवतरण यहीं से होता है और उसकी धारा सुविस्तृत भूखण्ड पर प्रवाहित हो चलती है। सद्ज्ञान का विस्तार सत्कर्म में होता है। सद्भावनाएं अवतरित होती हों और वे सत्प्रवृत्तियां बनकर कर्म क्षेत्र में बहती हो तो समझना चाहिए कि भक्त भागीरथ की तप साधना सफल हो चली और ईश्वर दर्शन का प्रयोजन पूर्ण हो गया।
अपने जीवन में ईश्वर की विद्यमानता देख सकना कुछ भी कठिन नहीं है। उत्कर्ष को आत्म गौरव को प्राप्त करने की आकांक्षा स्पष्टतः यही अंगुलि निर्देश करती है कि पशु स्तर का जीवन यापन अपर्याप्त है—अतृप्ति कर है—अवांछनीय है इस स्थिति से आगे बढ़ा जाय ऊंचा उठा जाय। मात्र जीवात्मा न रहकर महानात्मा—देवात्मा एवं परमात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया जाय। भटकाव के कारण यह लाभ भौतिक वस्तुएं समेटने और दूसरों को चमत्कृत करने वाले जादुई विलास वैभव के संग्रह में इस लक्ष्य की पूर्ति सोची जाती है। बड़प्पन के ठाठ रोपे जाते हैं और उस उन्माद में कुमार्ग अपना कर प्रगति के नाम पर पतन के गर्त में गिरा जाता है। यदि यथार्थता को समझा जा सके तो यह आत्मिक आकांक्षा सम्पन्नता संग्रह करने के लिए महानता सम्पादित करने के लिए मार्ग दर्शन करती दिखाई पड़ेगी। उत्कर्ष की उमंग के रूप में अपने भीतर हम ईश्वरीय सत्ता को दिशा निर्देश करती हुई देख सकते हैं।
विवेक के रूप में उचित को अपनाने और अनुचित से बचने की प्रक्रिया भी ईश्वर हर घड़ी पूरा करता है। प्रत्येक सत्कर्म हमें आन्तरिक सन्तोष देता है और प्रत्येक दुष्कर्म के प्रयास से छाती धड़कती है। अन्तर्द्वन्द्व खड़ा होता है और पैर कांपते हैं। औचित्य के लिए प्रोत्साहन देने वाले और अनौचित्य के प्रति निरुत्साह उत्पन्न करने वाले इस अन्तःप्रकाश को ईश्वरीय सत्ता की विद्यमानता के रूप में देखा जा सकता है।
करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा जैसी सद्भावनाएं असीम आत्म-संतोष प्रदान करती हैं। इन्हें चरितार्थ करने के लिए कुछ कष्ट सहना, संयम बरतना और त्याग करना पड़ता है तो भी उससे दुख नहीं संतोष ही होता है। इसे ईश्वरीय चेतना का दिव्य शिक्षण कह सकते हैं। उत्कृष्टता की भूख अदम्य है—न्याय और औचित्य का समर्थन शाश्वत है। चोर भी चोरी के सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर सकता—वह अपने घर चोर को नौकर रखने के लिए तैयार न होगा। यह सत्य की ईश्वरत्व की दिग्विजय है। हमने निरन्तर ईश्वरीय वाणी की अवज्ञा और प्रेरणा की अवहेलना की है सो आदत भी वैसी बन गयी है। धूलि जमते-जमते दर्पण धुंधला हो गया है अन्यथा हर कोई अन्तरात्मा के भीतर महानता की दिशा में बढ़ चलने की प्रेरणा के रूप में कोई भी कभी भी जीवन्त किन्तु धूमिल बनाई गई ईश्वरीय चेतना का दर्शन कर सकता है।
शरीर के ढांचे पर दृष्टि डाली जाय और उसके भीतर कार्यान्वित हो रही रीति नीति पर गहराई से ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि ईश्वरीय चेतना की प्रकृति क्या है और वह व्यष्टि एवं समष्टि में किस प्रकार काम करती है। घटकों की घनिष्ठता और अवयवों की सहकारिता देखते ही बनती है। यों जीवाणुओं की स्वतन्त्र सत्ता है पर उन सबने इस प्रकार का निर्वाह क्रम अपनाया है कि घनिष्ठता देखते ही बनती है। उलट पुलट कर देखा जाय तो वे एक दूसरे के साथ गुंथे हुए लगेंगे। उनमें से किसी की इच्छा अलग रहने या अलग बढ़ने की नहीं होती। हर घटक का संतोष पारिस्परिक आत्मीयता का आनन्द लेने में ही केन्द्रित हो रहा है। इनमें से किसी घटक को काटकर अलग किया जाय तो छोटी सी काट छांट भी सारे शरीर को व्यथित कर देती है और जहां से कुछ कटा था वहीं रक्त के आंसू बहने लगते हैं। प्रत्येक जीवाणु अहर्निशि श्रम निरत रहता है और अपनी सत्ता का लाभ समूचे शरीर को देता है। यह सघनता ईश्वरीय है। व्यक्ति को घटक बनकर रहना चाहिए और उसका स्वार्थ और परमार्थ एक रहना चाहिए।
अवयवों की सहकारिता दर्शनीय है। हाथ कमाता है—उस कमाई को मुंह खाता है—मुंह पेट में पहुंचाता है—पेट पचाकर रक्त बनाता है—रक्त हृदय के अधिकार में पहुंचता है और वहां से सारे शरीर में पहुंचता है। छोटी बड़ी नलिकाएं इस वितरण की समर्थक और सहायक बनकर रहती हैं। सामर्थ्य का अधिकाधिक उपयोग—उपभोग के लिए न्यूनतम से तुष्टि, यही है प्रत्येक छोटे बड़े अवयव की नीति। यह घाटे का सौदा नहीं है। हाथ ने कमा कर शरीर पोषण के लिए अपना समग्र उपार्जन समर्पित कर दिया, यह स्थूल दृष्टि के लिए घाटे का मूर्खता का काम था। पर वस्तुतः इसमें लाभ ही लाभ रहा। सुरक्षा की चिन्ता—अहंकार की उद्धतता-संग्रह की सड़न से बचत हो गई और उपार्जित अन्न धन-बहूमूल्य रक्त मांस बनकर हाथ के लिए वापिस आ गया। सूक्ष्म दर्शियों के लिए वह बुद्धिमत्ता का काम रहा। हाथ ने आदर्शवादिता का श्रेय प्राप्त किया और अन्यान्य अवयवों के सहयोग से रक्त का बहुमूल्य भंडार उपलब्ध कर लिया। यह ईश्वरीय रीति नीति है व्यक्ति और समाज के बीच वैसा ही सामंजस्य सौमनस्य रहना चाहिए जैसा कि शरीर को सुव्यवस्थित बनाये रहने के लिए ईश्वर ने अवयवों के बीच स्थापित किया है।
उपयोगी आवश्यक का गृहण अनुपयोगी अनावश्यक का परित्याग शरीर के निर्वाह क्रम का अविच्छिन्न अंग है। भोजन मिलता है उससे जो तत्व जितनी मात्रा में प्रयुक्त हो सकता है उतना ग्रहण कर लिया जाता है और शेष मल रूप में बाहर हटा दिया जाता है। संग्रह की तनिक भी उपयोगिता नहीं—संग्रह बढ़ेगा तो मलावरोध उत्पन्न होगा और सड़न से अनेकानेक रोग उठ खड़े होंगे। मल विसर्जन की क्रिया देखते ही बनती है। विकृतियां जहां भी उत्पन्न हों वहीं से उन्हें खदेड़ बाहर किया जाना चाहिए। शरीर में बड़े बड़े नौ छिद्र हैं वे सभी मल विसर्जन में निरत रहते हैं। त्वचा के असंख्य छिद्र पसीने के माध्यम से विकृतियों को बाहर खदेड़ते हैं। फेफड़े में जाने वाली हर सांस उत्पन्न हुए विषों को समेट कर लाती है और उन्हें बुहार कर बाहर फेंकती हैं। हमारे भीतर गुण कर्म स्वभाव के—शरीर मन और भावना के क्षेत्र में जहां भी—जब भी—लेने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रेष्ठ हो—उत्कृष्ट हो उसी को हम संग्रह करें और शेष को उपेक्षा के गर्त में धकेल कर बाहर करदें। इतना सहज शिक्षण ईश्वर की इस रीति-नीति को देखकर सीखा जा सकता है जो शरीर सत्ता के अन्तर्गत आजीवन काम करती रहती है।
जन्म से लेकर मरण पर्यन्त शरीर का सारा ढांचा श्रमशील रहता है। स्थिति बदल देना भर विश्राम है। हर अवयव अपनी नियत मर्यादा का पालन करता है और अपने जिम्मे का उत्तरदायित्व निवाहता है। कर्त्तव्यनिष्ठा-मर्यादाओं का पालन, उदार सहकारिता का निर्वाह—अविश्राम श्रमशीलता जैसी रीति नीति अपना कर ही शरीर का स्वास्थ्य—मन का संतुलन और अन्तःकरण का चरित्र स्थिर रखा जा सकता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के बलिष्ठ रहने का यही उपाय है। ईश्वर का कर्तृत्व शरीर के क्रिया कलाप के चल रहे विधि विधान को देखकर समझा जा सकता है अभक्ष्य पदार्थ खाने से उदरशूल रेचक से दस्त, नशा पीने पर उन्माद, विष पीने से मृत्यु, असावधानी से चलने पर ठोकर जैसे घटनाक्रमों को देखकर कर्म फल का सिद्धान्त समझा जा सकता है। अपने भीतर झांककर यदि देखा जा सके तो जिनकी चर्चा की गई है वे दो चार प्रसंग ही नहीं, असंख्यों आधार ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो ईश्वर की रीति नीति का दिग्दर्शन कराते हैं। चेतना सदा निराकार होती है इसलिए उसे चर्म चक्षुओं से तो नहीं देखा जा सकता पर ज्ञान नेत्रों से उसकी गति विधियों का दर्शन किया जा सकता है। यही है ईश्वर का साक्षात्कार। इसका प्रतिफल यही होना चाहिए कि हम अपनी व्यावहारिक रीति नीति का निर्धारण उसी आधार पर करना चाहिए जिसे ईश्वरीय सत्ता द्वारा अपनाया गया है। ईश्वर भक्ति का—उसका उपासना साधना का प्रयोजन यही है कि हम उसी राह पर चलें जो उसने हमारी प्रत्यक्ष पाठ्य पुस्तक में लिख दी है।
आन्तर क्षेत्र की तरह बाह्य जगत में भी ईश्वरीय सत्ता का दर्शन उसकी रीति नीति के रूप में देखते हुए किया जा सकता है। समुद्र में जमा रहने पर जल खारा रहता है और निरुपयोगी बनता है। कुछ ही समय में खाद बन जाता है। आततायी आपस में ही लड़ते मरते और समाप्त होते रहते हैं। अवांछनीयता अपनाने वाली असुरता सदा हारी और दैवी सत्ता ने अपना वर्चस्व घोर संघर्षों के बीच भी कायम रखा है। एक से एक बढ़कर अनाचारी आये और असीम घृणा एवं अनन्त अशान्ति लेकर महाकाल की करालता में समा गये पर बुद्ध और ईसा अभी भी जिन्दा हैं। शिवि, दधीचि हरिश्चंद्र की—ध्रुव प्रहलाद की—सूर कबीर की, मीरा और तुलसी की सत्ता अभी भी जीवित हैं। कालजयी महामानवों को इतिहास के पृष्ठों पर से मिटाया न जा सकेगा जब तक धरती और आसमान है तब तक महामानवों की देव सत्ता अमृत वाणी-अजर अमर बनी रहेगी और उनके चरण चिन्हों पर श्रद्धा के शत दल कमल मानवी आत्मा निरन्तर अर्पित करनी रहेगी।
उपभोग वादी संग्रही और आधिपत्य जताने वाले अतृप्ति और असंतोष का रोना रोते रहेंगे पर जिन्हें सौन्दर्य का बोध है वे नील आकाश के झिलमिलाते तारकों में रात भर—लहलहाती हरितमा में दिन भर दिव्य सौन्दर्य का अनुभव करते हुए हर घड़ी हर्षोल्लास में डूबे रहेंगे। चित्र विचित्र प्राणियों के चलते बोलते खिलौने कितने सुन्दर हैं। भोला बचपन इठलाता यौवन और परिपक्व वृद्धत्व कितना भावात्मक होता है इसे किसी भी कलाकार की आंखें देखतीं और ठगी सी रह जाती हैं। प्रकृति की छोटी बड़ी हलचलों को यदि भाव भरी आंखों से देखा जा सके तो प्रतीत होगा कि इस सृष्टि के कण कण से सौन्दर्य बरसता है—पारस्परिक स्नेह सहयोग का यहां कितना निर्मल प्रवाह बह रहा है। सत् की ये सत्ता चेतना के समुद्र में किस प्रकार क्रीड़ा कल्लोल कर रही है ये देखते ही बनता है। यहां सत चित और आनन्द के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। संघर्ष, पाप और संग्रह जहां भी होगा वहीं विकृत बनेगा और संकट उत्पन्न करेगा। बादल जल लाते हैं सूखे भूतल को सींचते हैं। उनका क्रिया कलाप उन्हें ऊंचा चढ़ाता है, देवता बनाता है, आगमन पर सर्वत्र मोद मनाया जाता है। बरसने पर भी वे खाली नहीं होते। हर वर्ष उनका अस्तित्व यथावत् बना रहता है। बादलों का पानी जमीन को मिलता है—जमीन से नदियों में नदियों से समुद्र में जा पहुंचता है। यह एक से दूसरे को देने की पद्धति ही सृष्टि को सुस्थिर और समुन्नत रखे हुए हैं। यदि रोक रखने की लोभ नीति अपनाई जाय, तो बादल क्यों बरसेंगे? जमीन अपनी नमी नदियों को क्यों देगी? नदियां सारा पानी अपने में भरे रहेंगी। संग्रह वृत्ति के अपनाने पर कितना बड़ा प्रकृति संकट उठ खड़ा होगा यह कल्पना करने मात्र से जी दहल जाता है। प्रकृति की हलचलों में ईश्वर के कर्तृत्व को यदि झांका जा सकेगा तो प्रभु दर्शन का प्रकाश हमें सहज ही मिल सकता है।
वनस्पति उगती है दूसरों के लिए, वृक्ष फलते हैं दूसरों के लिए, गाय दूध, भेड़ें ऊन, मक्खियां मधु देती हैं, फूल खिलते और सुगंध बिखेरते हैं—झरने झरते हैं और नदियां बहती हैं—धरती अपने असंख्य अनुदानों से प्राणियों का पोषण करती है। पवन चलता है—सूरज उगता है, चन्द्रमा चमकता है और तारे झिलमिलाते हैं। इन सबका अपना प्रत्यक्ष लाभ क्या है? ईश्वर ने स्वयं इस विशाल सृष्टि का उत्तरदायित्व क्यों संभाला हुआ है? इन प्रश्नों का उत्तर यदि खोजने के लिए उतरा जाय सृष्टि का कण कण उत्कृष्टता से ओत प्रोत हो रहा है और उसी के आधार पर इस विश्व का सूत्र संचालन हो रहा है। अवांछनीयताएं भी इस संसार में उत्पन्न होती हैं पर वे पनपने नहीं पातीं अपनी मौत मरती है और श्रेष्ठता की सघनता में उनका अस्तित्व टिक नहीं पाता। अंधेरा आता तो है पर प्रकाश के सन्मुख टिक नहीं पाता। प्राणियों द्वारा त्यागा दुर्गन्धित मल अनाचार की भी यहां सत्ता है पर वह है वहीं जहां ईश्वरीय सत्ता की न्यूनता है। संसार में कष्ट, शोक, सन्ताप, विद्वेष और विघटन की असुरता भी मिल सकती है पर वह कृति नहीं विकृति है। कृति और विकृति का संघर्ष भी उस परम पुरुष की एक स्फुरणा है जिसके सहारे असत पर सत् की—मरण पर जीवन की और अन्धकार पर प्रकाश की विजय की प्रत्यक्ष अनुभूति मिल सकती है।
ईश्वर का दर्शन—ईश्वर का अनुग्रह जीवन का लक्ष्य है। यह चर्म चक्षुओं से संभव नहीं। चमड़े के बने नेत्र तो केवल जड़ पदार्थों को देख सकते हैं, चेतना तो इन्द्रियातीत है, उसकी अनुभूति ज्ञान चक्षुओं से, विवेक दृष्टि से हो सकती है। अन्तरंग को खोजने और बहिरंग को निहारने से हमें ईश्वर की सत्ता का दर्शन हो सकता है। परमाणु के पटक अन्ततः विद्युत प्रवाह वे स्फुल्लिंग मात्र हैं। पदार्थ की मूल इकाई रासायनिक नहीं विद्युतीय है। शक्ति ही दृश्य का रूप धारण करती है यह समूचा पिंड और ब्रह्मांड ब्राह्मी सत्ता का कलेवर है। यहां सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म ज्योतिर्मय है। माया के आवरण ने उसके दर्शन आनन्द में व्यवधान उत्पन्न किया है। उपासना और साधना की छेनी हथोड़े से उसी अवरोध को नष्ट करने की हटाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है यदि इस तथ्य को समझा जा सके तो ईश्वर दर्शन की प्यास को सहज ही बुझा सकते हैं। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने उसकी प्रकृति और प्रेरणा को हृदयंगम कर लेने पर जो असीम आनन्द मिलता है, शक्तियों का अजस्र स्रोत हाथ लगता है, स्तर में देवत्व परिलक्षित होता है वही है जीव का चरम लक्ष्य और वही है परम पुरुषार्थ का महानतम प्रतिफल।
***