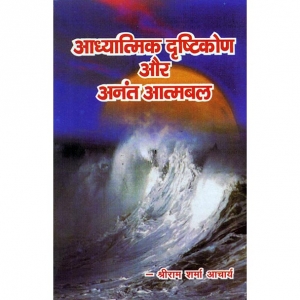अध्यात्म दृष्टिकोण और अनन्त आत्मबल 
अध्यात्म ही सभी समस्याओं के समाधान में सक्षम
Read Scan Version
वैयक्तिक कारणों से आये दिन होते रहने वाले लड़ाई झगड़ों से लेकर समाजों और वर्गों के मध्य चलने वाले संघर्ष क्यों उभरते हैं? आक्रमण-प्रत्याक्रमणों का कुचक्र क्यों गतिशील रहता है? देश-देशों के बीच युद्ध क्यों होते हैं? इसके कारणों पर शोधकर्त्ताओं ने मनोविज्ञान को आधारभूत माना है। यों लड़ाइयों के छोटे-मोटे कारण सामयिक भी होते हैं, पर वे ऐसे नहीं होते जो वार्तालाप, समझौता, उदारता अथवा न्याय निर्णय के आधार पर हल न हो सकते हों। अत्यन्त गम्भीर कारणों से उत्पन्न होने वाले विग्रहों तक के जब समाधान खोज निकाले जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि तनिक सी बात पर इतना विग्रह उभरे, जिससे चिरकाल तक वातावरण विक्षुब्ध बना रहे और धन-जन की असाधारण हानि सहन करनी पड़े।
पिछली पीढ़ी के नृतत्व वेत्ता यह मानते रहे हैं कि मनुष्य की डरपोक प्रवृत्ति, किसी प्रतिपक्षी के भयंकर आक्रमण की आशंका से ग्रसित हो जाती है तो अपने ऊपर भयंकर विपत्ति टूटने की कल्पना करने लगती है। डर बढ़ता है। उस काल्पनिक आक्रमण को रोकने के लिए बचाव की रक्षा पंक्ति खड़ी करने के रूप में प्रतिपक्षी को दुर्बल बनाने की दृष्टि से छोटा आक्रमण किया जाता है। आक्रमण का प्रत्युत्तर प्रत्याक्रमण के रूप में मिलता है। फलतः यह कुचक्र चक्रवृद्धि क्रम से घूमता है और कुछ ही समय में तिल का ताड़ बन जाता है। चिनगारी भयानक अग्नि काण्ड का रूप धारण कर लेती है।
मनोविज्ञानी एक और भी कारण बताते हैं कि हर मनुष्य में अपनी विशेषता और बलिष्ठता सिद्ध करने की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होती है। उसे पूरा करने का सहज तरीका तो अपनी योग्यता एवं सफलता सिद्ध करने का ही हो सकता है पर उसके लिए जिस दृढ़ता, तत्परता और कुशलता की आवश्यकता होती है वह जुट नहीं पाती। ऐसी दशा में हानि पहुंचाने की क्षमता प्रदर्शित करने का आतंकवादी तरीका अपनाना पड़ता है। इसी में शौर्य पराक्रम समझा जाता है। आक्रमण करके दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी सामर्थ्य सिद्ध करना भी लड़ाइयों की तरह ही एक बड़ा कारण होता है। बहाना तो किसी छोटे मोटे अप्रिय प्रसंग का ही ले लिया जाता है।
अपराधियों की दुष्टताएं इससे भिन्न हैं जो चोरी, डकैती, हत्या बलात्कार की—उद्दण्डता बरतने और मर्यादाएं तोड़ने के रूप में सामने आती रहती हैं। उनमें अर्थ लोभ, एवं द्वेष बुद्धि की प्रधानता रहती है। दुस्साहस का अहंकार भी उसमें जुड़ा रहता है।
नई पीढ़ी के वैज्ञानिक कहते हैं—युद्ध मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। स्वभावतः मनुष्य सामाजिक और सहयोगी प्रकृति का है, उसे सुविधा और खुशी चाहिए। युद्ध में आघात प्रत्याघात से हर दृष्टि से हानि ही हानि उठानी पड़ती है। जीतने वाला भी घाटे में ही रहता है। ऐसी दशा में युद्ध को स्वाभाविक प्रकृति नहीं माना जा सकता है, वह कुसंस्कारों एवं विकृत वातावरण की प्रतिक्रिया ही माना जा सकता है।
अहंमन्यता का विकृत रूप उद्दंडता है, जिसकी ओछी पूर्ति दूसरों का तिरस्कार करके की जा सकती है। झगड़ालू स्वभाव में यही तथ्य काम करता है। यदि मनुष्य को आरम्भ से ही शिष्टता, शालीनता, नम्रता और नागरिकता की शिक्षा दी जाय तो वह आक्रमण की अपेक्षा दूसरों की सहायता करने और बदले में श्रेय सम्मान पाने की बात सोचेगा। ऐसी दशा में मतभेद और स्वार्थ विपर्यय होते हुए भी ऐसा मार्ग खोज लिया जायगा जिसमें झंझट कम खड़ा हो और गुत्थी शान्ति में सुलझ जाय।
पक्षपात की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी ही विग्रह की सम्भावना बढ़ेगी। उचित अनुचित का भेद कर सकना तथ्य को ढूंढ़ना और न्याय की मांग को सुन सकना पक्षपात के आवेश में सम्भव ही नहीं हो पाता। अपने वर्ग की अच्छाइयां ही दीखती हैं और प्रतिपक्षी की बुराइयां ही सामने रहती हैं। अपनों की भूलें और विरानों के न्याय तथ्य भी समझ में नहीं आते। तब एक पक्षीय चिन्तन उद्धत बन जाता है। ऐसी दशा में आक्रमण प्रत्याक्रमण का क्रम चल पड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि तथ्यों को खोज निकालने की दूरदर्शिता अपनाये रहा जाय, कारणभूत तथ्यों को ढूंढ़ निकाला जाय और न्यायोचित समाधान के लिए प्रयास किया जाय तो तीन चौथाई लड़ाइयां सहज ही निरस्त हो सकती हैं। न्याय, और औचित्य को अपनाने वाली उदार सद्भावना का विकास हो सके तो युद्ध प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है। विग्रह की चिनगारी अन्ततः कितने बड़े दुष्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है इस पर सही ढंग से विचार किया जा सके तो विग्रह की हानि और समाधान का सत्परिणाम सोचा जा सकेगा। ऐसी दशा में युद्ध से बचे रहने की प्रवृत्ति पनपेगी और शान्ति का पक्ष मजबूत होता चला जायगा।
वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष उत्पन्न कराने वाले कारणों को निरस्त न किया जा सके तो कम से कम उनकी उपेक्षा तो होनी ही चाहिए। सहयोग और समीपता के सूत्र तथा आधार ढूंढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा जाना चाहिए। सम्प्रदाय, भाषा, जाति, वर्ग, क्षेत्र, देश आदि के नाम पर उभरने वाली भेद बुद्धि को यथा सम्भव हटाने या घटाने का प्रयत्न चलना चाहिए। कम से कम इन मतभेदों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने और दूसरों की तुलना में, विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न तो नहीं ही किया जाय। अपनी मान्यताओं के प्रति निष्ठावान रहना ठीक है पर उनका प्रदर्शन इस प्रकार नहीं होना चाहिए जिससे अन्य मान्यताओं का तिरस्कार होता हो। धर्म के नाम पर आये दिन कलह इसीलिए होते हैं कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसकी विशेषता बताने की अपेक्षा अन्यों की निकृष्टता सिद्ध करके अपना बड़प्पन सिद्ध करने का घटिया तरीका अपनाया जाता है। यही बात जातिगत श्रेष्ठता एवं देश-देश के बीच चलती रहती है। यदि दूसरों का—मनुष्यों और वर्गों का सम्मान करने का ध्यान रखा जाय तो समन्वय, सहिष्णुता एवं सद्भावना के वातावरण में संसार में पायी जाने वाली अनेकों भिन्नताएं बिना टकराये अपने-अपने ढंग पनपती रह सकती हैं और एक दूसरे के लिए सहयोगी एवं पूरक सिद्ध हो सकती हैं। संघर्ष का एक ही केन्द्रबिन्दु रहे—अनैतिकता-असामाजिकता। इसके लिए वर्ग संघर्ष को नहीं समूची मानवता के संयुक्त रूप से टूट पड़ने की मुहीम खड़ी की जानी चाहिए।
प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति यदि स्वाभाविक है तो श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खेल-कूद स्वास्थ्य संवर्धन, शिक्षा, कला आदि में विशेषता, उदार सेवा साधना जैसे अनेक क्षेत्र ढूंढ़े जा सकते हैं जिनमें लोग अपनी विशेषता बिना दूसरों का तिरस्कार किये या कष्ट पहुंचाये ही सिद्ध कर सकें।
उदार मनोवृत्ति अपनाकर ही चैन से रहने और रहने देने की स्थिति बनती है। उदारता का अर्थ दान पुण्य ही नहीं है वरन् यह भी है कि संकीर्ण दृष्टि से सोचना बन्द किया जाय और दूसरों की स्थिति में अपने आपको रख कर यह सोचा जाय कि गलतफहमी कहां है? और कहीं पक्षपात अथवा अनौचित्य को प्रश्रय तो नहीं मिला है। न्याय और विवेक की कसौटी अपनाकर वस्तुस्थिति को समझना अधिक अच्छी तरह सम्भव हो सकता है। प्यार और सहयोग पर यदि अपना विश्वास हो तो संघर्ष की कम ही आवश्यकता पड़ेगी। फिर अनिवार्यतः जो झंझट करना भी पड़ेगा उसकी न तो बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी और न द्वेष का कुचक्र देर तक चलता रह सकेगा। यह उदार, गम्भीर, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण मनोवृत्ति विकसित करना ही अध्यात्मिक विकास है।
दुष्प्रवृत्तियों के भार से लदा-दबा चित आध्यात्मिक न होगा, न हो सकता है। इस अध:स्थिति से ऊपर उठना ही आंतरिक विकास का आरम्भ है। भारीपन, जड़ता, तमोगुण के पर्याय कहे जाते हैं। जबकि हलकापन और प्रकाश सत्वगुण के लक्षण हैं। सत्वगुण के विकास से, आंतरिक स्तर ऊपर उठाने के अभ्यास से ही अध्यात्मिक प्रयोजन सध सकता है।
शरीर क्या है? मल-मूत्र से भरा और हाड़-मांस से बना घिनौना किन्तु चलता-फिरता पुतला। जीव क्या है—आपाधापी में निरत, दूसरों को नोंच खाने की कुटिलता में संलग्न—चेतना स्फुल्लिंग। जीवन क्या है—एक लदा हुआ भार जिसे कष्ट और खीज के साथ ज्यों-त्यों कर के वहन करना पड़ता है। बुलबुले की तरह एक क्षण उठना और दूसरे क्षण समाप्त हो जाना यही है जीवन की विडम्बना, जिसे असन्तोष और उद्वेग की आग में जलते-जलते गले में बांधे फिरना पड़ता है। स्थूल तक ही सीमित रहना हो तो इसी का नाम जीवन है। पेट और प्रजनन ही इसका लक्ष्य है। लिप्सा और लोलुपता की खाज खुजाते रहना ही यहां प्रिय प्रसंग है। आत्म-रक्षा, अहन्ता, मुक्ति की आतुरता, स्वामित्व की तृष्णा यही हैं वे सब मूल प्रवृत्तियां जिनसे बंधा हुआ प्राणी कीट-मरकट की तरह देखा जाता है। स्थूल जीवन को यदि देखना-परखना हो तो इस प्रवंचना के अतिरिक्त यहां और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भूल-भुलैयों की उलझनें इतनी पेचीदा होती हैं कि उन्हें सुलझाने का जितना प्रयत्न किया जाता है उलटे उतनी ही कसती चली जाती हैं। रोता जन्म लेता है और रुलाते हुए विदा होता है—यही है वह सब जिसे हम जीवन के नाम से पुकारते हैं।
वस्तुतः जीवन इतना तुच्छ, जटिल और घिनौना है नहीं। उसकी यथार्थता का मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। समुद्र की ऊपरी सतह पर तो कूड़ा-करकट, झागफेन, काई शैवाल, लहरों की उठक-पटक के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया जा सकता। रत्न राशि तो समुद्र तल में पड़ी होती हैं। उसे पाने के लिए गहराई में उतरने वाले गोताखोरों जैसा कौशल और साहस संजोना पड़ता है।
चेतना का स्थूल क्षेत्र पदार्थ—परिस्थिति और आतुरता भरी हलचलों में देखा जा सकता है। यह पशु जीवन है और प्रत्येक प्राणी को समान रूप से उपलब्ध है। जिसे जिस स्तर की काया मिली है वह उतने में ही अपने ढंग से रोता-गाता गुजर कर लेता है। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। क्रिया में दौड़-धूप की उत्तेजना भर है, नशे में भी उत्तेजना होती है और कई लोग उसे भी आनन्द और सन्तोष का माध्यम बना लेते हैं। समझना एक बात है और यथार्थता दूसरी। कुछ को कुछ भी समझा जा सकता है, पर उन भ्रान्ति से बनता तो कुछ नहीं। स्थिती तो स्थिति ही रहती है। आनन्द सूक्ष्म में है। क्रिया से नहीं, विचारणा से हमारा समाधान होता है और भावना की गहराई में उतरने से आनन्द का निर्झर फूट पड़ता है। यदि समाधान—तृप्ति एवं सन्तोष अभीष्ट हो तो क्रियाशील रहते हुए भी हमें ज्ञानवान बनना पड़ेगा। ज्ञान का आश्रय लिए बिना, दिग्भ्रान्ति स्थिति में आशंका और उद्विग्नता ही छाई रहेगी। शान्ति तो समाधान में है, वह समाधान सद्ज्ञान का आश्रय लिए बिना अन्य किसी आधार पर हो नहीं सकती।
क्रिया स्थूल है और ज्ञान सूक्ष्म। क्रिया तक सीमित न रहकर, तत्व चिन्तन की गहराई में उतरने के प्रयत्न में, हमें चैन और सन्तोष मिलता है। एक परत इससे भी गहरी है—जिसे अन्तरात्मा कहते हैं। यहां आस्थाएं रहती हैं। अपने सम्बन्ध में, प्रिय और अप्रिय के, उचित और अनुचित के, आदतों और प्रचलनों के, पक्ष और सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अनेकानेक मान्यताएं, इसी केन्द्र में गहराई तक जड़े जमाए बैठी रहती हैं। व्यक्तित्व का समूचा ढांचा, यहीं विनिर्मित होता है। मस्तिष्क और शरीर को तो व्यर्थ ही दोष या श्रेय दिया जाता है। वे दोनों ही वफादार सेवक की तरह हर आत्मा की ड्यूटी ठीक तरह बजाते रहते हैं। उनमें अवज्ञा करने की कोई शक्ति नहीं। आस्थाएं ही प्रेरणा देती हैं और उसी पैट्रोल से धकेले जाने पर जीवन स्कूटर के दोनों पहिये—चिन्तन और कर्तृत्व सरपट दौड़ने लगते हैं। व्यक्तित्व क्या है—आस्था। मनुष्य क्या है—श्रद्धा। चेष्टाएं क्या हैं—आकांक्षा की प्रतिध्वनि। गुण, कर्म, स्वभाव अपने आप न बनते हैं न बिगड़ते हैं। आस्थाएं ही आदतें बनकर परिपक्व हो जाती हैं तो उन्हें स्वभाव कहते हैं। अभ्यासों को ही गुण कहते हैं। कर्म आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शरीर और मन को संयुक्त रूप से जो श्रम करना पड़ता है, उसी को कर्म कहते हैं। इन तथ्यों को समझ लेने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के स्तर और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले सुख-दुःखों की अनुभूति होती रही है। प्रसन्नता और उद्विग्नता को यों परिस्थितियों के उतार-चढ़ावों से जोड़ा जाता है, पर वस्तुतः वे मनःस्थिति के सुसंस्कृत और अनगढ़ होने के कारण सामान्य जीवन में नित्य ही आती रहने वाली घटनाओं से ही उत्पन्न अनुभूतियां भर होती हैं। कोई घटना न अपने आप में महत्वपूर्ण है और न महत्व हीन। यहां सब कुछ अपने ढर्रे पर लुढ़क रहा है। सर्दी-गर्मी की तरह भाव और अभाव का, जन्म-मरण और हानि-लाभ का क्रम चलता रहता है। हमारे चिन्तन का स्तर ही उनमें कभी प्रसन्नता अनुभव करता और कभी उद्विग्न हो उठता है। अनुभूतियों में परिस्थितियां नहीं, मनःस्थिति की भूमिका ही काम करती है।
जीवन के सफेद और काले पक्ष को समझ लेने के उपरान्त, सहज ही प्रश्न उठता है कि—क्या ऐसा सम्भव नहीं है कि परिस्थितियों के ढांचे में ढले—लोक-प्रवाह में बहते हुए, संग्रहीत कुसंस्कारों से प्रेरित, वर्तमान अनगढ़ जीवन को, अपनी इच्छानुसार—अपने स्तर को फिर से गढ़ा जाय और प्रस्तुत निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदल दिया जाय? उत्तर ‘ना’ और ‘हां’ दोनों में दिया जा सकता है। ‘ना’ उस परिस्थिति में जब आन्तरिक परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा का अभाव हो और उसके लिए आवश्यक साहस जुटाने की उमंगें उठती न हों। दूसरों की कृपा सहायता के बलबूते उज्ज्वल भविष्य के सपने तो देखे जा सकते हैं, पर वे पूरे कदाचित ही कभी किसी के होते हैं। बाहरी, दैवी और संसारी सहायताएं मिलती तो हैं, पर उन्हें पाने के लिए पात्रता की अग्नि-परीक्षा में गुजरते हुए अपनी प्रामाणिकता का परिचय देना पड़ता है। उतना झंझट सिर पर उठाने का मन न हो—सहज ही कुछ इधर-उधर की ‘हथफेरी’ करके भौतिक सम्पदाएं, आत्मिक विभूतियां पाने के लिए जी ललचाता भर हो तो कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व को महामानवों के स्तर पर गठित करना और उसके फलस्वरूप उच्चस्तरीय सिद्धियां प्राप्त कर सकना एक प्रकार से असम्भव ही है। उत्तर नकारात्मक समझा जा सकता है।
‘हां’ उस स्थिति में कहा जा सकता है जबकि साधक में यह विश्वास उभरा हो कि वह अपना स्वामी आप है—अपने भाग्य का निर्माण कर सकना उसके अपने हाथ की बात है। दूसरों पर न सही अपने शरीर और मन पर तो अपना अधिकार है ही और उसके अधिकार का उपयोग करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व हस्तक्षेप कहीं से भी नहीं हो सकता। मन की दुर्बलता ही है जो ललचाती, भ्रमाती और गिरती है। तनकर खड़ा हो जाने पर भीतरी और बाहरी सभी दबाव समाप्त हो जाते हैं और अभीष्ट दिशा में निर्भयता एवं निश्चिन्तता के साथ बढ़ा जा सकता है। समुद्र की गहराई में उतरकर मोती ढूंढ़ने में विशिष्ट प्रकार के साधन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जीवन समुद्र की गहराई में उतरकर एक से एक बहुमूल्य रत्न ढूंढ़ लाना सरल है। इसमें किसी बाहरी साधना या उपकरण की जरूरत नहीं—मात्र प्रचण्ड संकल्प शक्ति चाहिए। प्रचण्ड का तात्पर्य है धैर्य और साहस का उतनी मात्रा में समन्वय जिससे संकल्प के डगमगाते रहने की बाल बुद्धि उभर आने की आशंका न हो। स्थिर बुद्धि से सतत् प्रयत्न करते रहने और फल प्राप्ति में देर होते देखकर अधीर न होने की—वरन् दूने उत्साह से प्रयत्न करने की सजीवता जहां भी होगी वहां सफलता पैर चूमने के लिए हाथ जोड़े-सिर झुकाए खड़ी होगी। ऐसे मनस्वी व्यक्ति अपने को, अपने वातावरण का यहां तक कि, अपने प्रभाव क्षेत्र को कायाकल्प की तरह बदल सकने में सफल हो सकते हैं। जीवन परिष्कार की भविष्यवाणी करते हुए ऐसे ही लोगों की सफल सम्भावना को ‘हां’ कहकर आश्वस्त किया जा सकता है।
आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए न तो सही मार्ग जानते हैं और न उस पर चलने के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा पाते हैं। दिग्भ्रान्त प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? अन्धा अन्धे को कहां पहुंचा सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? आज की यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्मविज्ञान का न तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और न उसका क्रिया पक्ष—साधन विधान ही निःभ्रांति है। इस उलझन में एक सत्यान्वेषी जिज्ञासु को निराशा ही लगती है।
हमें यहां अध्यात्म के मौलिक सिद्धान्तों को समझना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगढ़ तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठापित करना है, जिसके आलोक में जीवन को सच्चे अर्थों में विकसित एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसके लिए मान्यता और क्रिया क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे क्या हों, किस प्रकार हों, इस शिक्षण में थ्योरी और प्रेक्टिस के दोनों ही अवलम्बन साथ-साथ लेकर चलना होता है। थ्योरी का तात्पर्य वह है सद्ज्ञान, वह आस्था विश्वास जो जीवन को उच्चस्तरीय लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए सहमत कर सके। इसे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान और सद्ज्ञान के नामों से जाना समझा जाता है—योग इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या का तत्वदर्शन यही है। प्रेक्टिस—का तात्पर्य है वे साधन विधान जो हमारी क्रियाशीलता को दिशा देते हैं और बताते हैं कि जीवनयापन की रीति-नीति क्या होनी चाहिए और गतिविधियां किस क्रम से निर्धारित की जानी चाहिए? साधनात्मक क्रिया-कृत्यों का यह उद्देश्य समझ लिया जाय तो फिर किसी को भी न तो अनावश्यक आशा बांधनी पड़ेगी और न अवांछनीय रूप में निराश होना पड़ेगा।
यह तथ्य हजार बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि जीवन का परम श्रेयस्कर और शान्तिदायक उत्कर्ष आस्थाओं के परिष्कार—चिन्तन के निखार एवं गतिविधियों के सुधार पर निर्भर है। जीवन इन्हीं तीन धाराओं में प्रवाहित होता है। शक्ति के स्रोत इन्हीं में भरे पड़े हैं। और अद्भुत उपलब्धियां उन्हीं में से उद्भूत होती हैं। इन्हें किस आधार पर सुधारा, संभाला जाय इसकी एक विशिष्ट पद्धति है अपने अन्तरंग और बहिरंग को उच्च स्तर तक उठा ले चलना। इसे जीवन का अभिनव निर्माण एवं व्यक्तित्व का कायाकल्प भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे योगाभ्यास तपश्चर्या कहते हैं।
चेतना का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने को योग समझा जाय। क्रियाकलाप में सुव्यवस्था का आरोपण तप माना जाय। इसके लिए कई तरह के प्रयोगात्मक अभ्यास करने पड़ते हैं। पहलवान बनने के लिए अखाड़े में जाकर छोटी-छोटी कसरतों का सिलसिला शुरू करना पड़ता है। कसरतों की खिलवाड़ और दंगल में कुश्ती पछाड़ कर यशस्वी होना दो अलग स्थितियां हैं, पर दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। बीज बोने का शुभारम्भ कालान्तर में विशाल वृक्ष बनकर सामने आता है। पूजा-उपासना और स्वाध्याय मनन जैसे उपचार बीजारोपण की तरह हैं जो खाद, पानी, निराई, गुड़ाई रखवाली आदि की चिरकाल तक अपेक्षा करते हैं और समयानुसार कल्पवृक्ष बनकर मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाते हैं। आन्तरिक दृष्टि से आनन्द-विभोर और बहिरंग दृष्टि से श्रद्धा का पात्र बना हुआ भूदेव यह अनुभव करता है कि आत्म-विज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और संसार का सबसे बड़ा लाभ है।
पिछली पीढ़ी के नृतत्व वेत्ता यह मानते रहे हैं कि मनुष्य की डरपोक प्रवृत्ति, किसी प्रतिपक्षी के भयंकर आक्रमण की आशंका से ग्रसित हो जाती है तो अपने ऊपर भयंकर विपत्ति टूटने की कल्पना करने लगती है। डर बढ़ता है। उस काल्पनिक आक्रमण को रोकने के लिए बचाव की रक्षा पंक्ति खड़ी करने के रूप में प्रतिपक्षी को दुर्बल बनाने की दृष्टि से छोटा आक्रमण किया जाता है। आक्रमण का प्रत्युत्तर प्रत्याक्रमण के रूप में मिलता है। फलतः यह कुचक्र चक्रवृद्धि क्रम से घूमता है और कुछ ही समय में तिल का ताड़ बन जाता है। चिनगारी भयानक अग्नि काण्ड का रूप धारण कर लेती है।
मनोविज्ञानी एक और भी कारण बताते हैं कि हर मनुष्य में अपनी विशेषता और बलिष्ठता सिद्ध करने की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होती है। उसे पूरा करने का सहज तरीका तो अपनी योग्यता एवं सफलता सिद्ध करने का ही हो सकता है पर उसके लिए जिस दृढ़ता, तत्परता और कुशलता की आवश्यकता होती है वह जुट नहीं पाती। ऐसी दशा में हानि पहुंचाने की क्षमता प्रदर्शित करने का आतंकवादी तरीका अपनाना पड़ता है। इसी में शौर्य पराक्रम समझा जाता है। आक्रमण करके दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी सामर्थ्य सिद्ध करना भी लड़ाइयों की तरह ही एक बड़ा कारण होता है। बहाना तो किसी छोटे मोटे अप्रिय प्रसंग का ही ले लिया जाता है।
अपराधियों की दुष्टताएं इससे भिन्न हैं जो चोरी, डकैती, हत्या बलात्कार की—उद्दण्डता बरतने और मर्यादाएं तोड़ने के रूप में सामने आती रहती हैं। उनमें अर्थ लोभ, एवं द्वेष बुद्धि की प्रधानता रहती है। दुस्साहस का अहंकार भी उसमें जुड़ा रहता है।
नई पीढ़ी के वैज्ञानिक कहते हैं—युद्ध मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। स्वभावतः मनुष्य सामाजिक और सहयोगी प्रकृति का है, उसे सुविधा और खुशी चाहिए। युद्ध में आघात प्रत्याघात से हर दृष्टि से हानि ही हानि उठानी पड़ती है। जीतने वाला भी घाटे में ही रहता है। ऐसी दशा में युद्ध को स्वाभाविक प्रकृति नहीं माना जा सकता है, वह कुसंस्कारों एवं विकृत वातावरण की प्रतिक्रिया ही माना जा सकता है।
अहंमन्यता का विकृत रूप उद्दंडता है, जिसकी ओछी पूर्ति दूसरों का तिरस्कार करके की जा सकती है। झगड़ालू स्वभाव में यही तथ्य काम करता है। यदि मनुष्य को आरम्भ से ही शिष्टता, शालीनता, नम्रता और नागरिकता की शिक्षा दी जाय तो वह आक्रमण की अपेक्षा दूसरों की सहायता करने और बदले में श्रेय सम्मान पाने की बात सोचेगा। ऐसी दशा में मतभेद और स्वार्थ विपर्यय होते हुए भी ऐसा मार्ग खोज लिया जायगा जिसमें झंझट कम खड़ा हो और गुत्थी शान्ति में सुलझ जाय।
पक्षपात की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी ही विग्रह की सम्भावना बढ़ेगी। उचित अनुचित का भेद कर सकना तथ्य को ढूंढ़ना और न्याय की मांग को सुन सकना पक्षपात के आवेश में सम्भव ही नहीं हो पाता। अपने वर्ग की अच्छाइयां ही दीखती हैं और प्रतिपक्षी की बुराइयां ही सामने रहती हैं। अपनों की भूलें और विरानों के न्याय तथ्य भी समझ में नहीं आते। तब एक पक्षीय चिन्तन उद्धत बन जाता है। ऐसी दशा में आक्रमण प्रत्याक्रमण का क्रम चल पड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि तथ्यों को खोज निकालने की दूरदर्शिता अपनाये रहा जाय, कारणभूत तथ्यों को ढूंढ़ निकाला जाय और न्यायोचित समाधान के लिए प्रयास किया जाय तो तीन चौथाई लड़ाइयां सहज ही निरस्त हो सकती हैं। न्याय, और औचित्य को अपनाने वाली उदार सद्भावना का विकास हो सके तो युद्ध प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है। विग्रह की चिनगारी अन्ततः कितने बड़े दुष्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है इस पर सही ढंग से विचार किया जा सके तो विग्रह की हानि और समाधान का सत्परिणाम सोचा जा सकेगा। ऐसी दशा में युद्ध से बचे रहने की प्रवृत्ति पनपेगी और शान्ति का पक्ष मजबूत होता चला जायगा।
वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष उत्पन्न कराने वाले कारणों को निरस्त न किया जा सके तो कम से कम उनकी उपेक्षा तो होनी ही चाहिए। सहयोग और समीपता के सूत्र तथा आधार ढूंढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा जाना चाहिए। सम्प्रदाय, भाषा, जाति, वर्ग, क्षेत्र, देश आदि के नाम पर उभरने वाली भेद बुद्धि को यथा सम्भव हटाने या घटाने का प्रयत्न चलना चाहिए। कम से कम इन मतभेदों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने और दूसरों की तुलना में, विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न तो नहीं ही किया जाय। अपनी मान्यताओं के प्रति निष्ठावान रहना ठीक है पर उनका प्रदर्शन इस प्रकार नहीं होना चाहिए जिससे अन्य मान्यताओं का तिरस्कार होता हो। धर्म के नाम पर आये दिन कलह इसीलिए होते हैं कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसकी विशेषता बताने की अपेक्षा अन्यों की निकृष्टता सिद्ध करके अपना बड़प्पन सिद्ध करने का घटिया तरीका अपनाया जाता है। यही बात जातिगत श्रेष्ठता एवं देश-देश के बीच चलती रहती है। यदि दूसरों का—मनुष्यों और वर्गों का सम्मान करने का ध्यान रखा जाय तो समन्वय, सहिष्णुता एवं सद्भावना के वातावरण में संसार में पायी जाने वाली अनेकों भिन्नताएं बिना टकराये अपने-अपने ढंग पनपती रह सकती हैं और एक दूसरे के लिए सहयोगी एवं पूरक सिद्ध हो सकती हैं। संघर्ष का एक ही केन्द्रबिन्दु रहे—अनैतिकता-असामाजिकता। इसके लिए वर्ग संघर्ष को नहीं समूची मानवता के संयुक्त रूप से टूट पड़ने की मुहीम खड़ी की जानी चाहिए।
प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति यदि स्वाभाविक है तो श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खेल-कूद स्वास्थ्य संवर्धन, शिक्षा, कला आदि में विशेषता, उदार सेवा साधना जैसे अनेक क्षेत्र ढूंढ़े जा सकते हैं जिनमें लोग अपनी विशेषता बिना दूसरों का तिरस्कार किये या कष्ट पहुंचाये ही सिद्ध कर सकें।
उदार मनोवृत्ति अपनाकर ही चैन से रहने और रहने देने की स्थिति बनती है। उदारता का अर्थ दान पुण्य ही नहीं है वरन् यह भी है कि संकीर्ण दृष्टि से सोचना बन्द किया जाय और दूसरों की स्थिति में अपने आपको रख कर यह सोचा जाय कि गलतफहमी कहां है? और कहीं पक्षपात अथवा अनौचित्य को प्रश्रय तो नहीं मिला है। न्याय और विवेक की कसौटी अपनाकर वस्तुस्थिति को समझना अधिक अच्छी तरह सम्भव हो सकता है। प्यार और सहयोग पर यदि अपना विश्वास हो तो संघर्ष की कम ही आवश्यकता पड़ेगी। फिर अनिवार्यतः जो झंझट करना भी पड़ेगा उसकी न तो बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी और न द्वेष का कुचक्र देर तक चलता रह सकेगा। यह उदार, गम्भीर, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण मनोवृत्ति विकसित करना ही अध्यात्मिक विकास है।
दुष्प्रवृत्तियों के भार से लदा-दबा चित आध्यात्मिक न होगा, न हो सकता है। इस अध:स्थिति से ऊपर उठना ही आंतरिक विकास का आरम्भ है। भारीपन, जड़ता, तमोगुण के पर्याय कहे जाते हैं। जबकि हलकापन और प्रकाश सत्वगुण के लक्षण हैं। सत्वगुण के विकास से, आंतरिक स्तर ऊपर उठाने के अभ्यास से ही अध्यात्मिक प्रयोजन सध सकता है।
शरीर क्या है? मल-मूत्र से भरा और हाड़-मांस से बना घिनौना किन्तु चलता-फिरता पुतला। जीव क्या है—आपाधापी में निरत, दूसरों को नोंच खाने की कुटिलता में संलग्न—चेतना स्फुल्लिंग। जीवन क्या है—एक लदा हुआ भार जिसे कष्ट और खीज के साथ ज्यों-त्यों कर के वहन करना पड़ता है। बुलबुले की तरह एक क्षण उठना और दूसरे क्षण समाप्त हो जाना यही है जीवन की विडम्बना, जिसे असन्तोष और उद्वेग की आग में जलते-जलते गले में बांधे फिरना पड़ता है। स्थूल तक ही सीमित रहना हो तो इसी का नाम जीवन है। पेट और प्रजनन ही इसका लक्ष्य है। लिप्सा और लोलुपता की खाज खुजाते रहना ही यहां प्रिय प्रसंग है। आत्म-रक्षा, अहन्ता, मुक्ति की आतुरता, स्वामित्व की तृष्णा यही हैं वे सब मूल प्रवृत्तियां जिनसे बंधा हुआ प्राणी कीट-मरकट की तरह देखा जाता है। स्थूल जीवन को यदि देखना-परखना हो तो इस प्रवंचना के अतिरिक्त यहां और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भूल-भुलैयों की उलझनें इतनी पेचीदा होती हैं कि उन्हें सुलझाने का जितना प्रयत्न किया जाता है उलटे उतनी ही कसती चली जाती हैं। रोता जन्म लेता है और रुलाते हुए विदा होता है—यही है वह सब जिसे हम जीवन के नाम से पुकारते हैं।
वस्तुतः जीवन इतना तुच्छ, जटिल और घिनौना है नहीं। उसकी यथार्थता का मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। समुद्र की ऊपरी सतह पर तो कूड़ा-करकट, झागफेन, काई शैवाल, लहरों की उठक-पटक के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया जा सकता। रत्न राशि तो समुद्र तल में पड़ी होती हैं। उसे पाने के लिए गहराई में उतरने वाले गोताखोरों जैसा कौशल और साहस संजोना पड़ता है।
चेतना का स्थूल क्षेत्र पदार्थ—परिस्थिति और आतुरता भरी हलचलों में देखा जा सकता है। यह पशु जीवन है और प्रत्येक प्राणी को समान रूप से उपलब्ध है। जिसे जिस स्तर की काया मिली है वह उतने में ही अपने ढंग से रोता-गाता गुजर कर लेता है। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। क्रिया में दौड़-धूप की उत्तेजना भर है, नशे में भी उत्तेजना होती है और कई लोग उसे भी आनन्द और सन्तोष का माध्यम बना लेते हैं। समझना एक बात है और यथार्थता दूसरी। कुछ को कुछ भी समझा जा सकता है, पर उन भ्रान्ति से बनता तो कुछ नहीं। स्थिती तो स्थिति ही रहती है। आनन्द सूक्ष्म में है। क्रिया से नहीं, विचारणा से हमारा समाधान होता है और भावना की गहराई में उतरने से आनन्द का निर्झर फूट पड़ता है। यदि समाधान—तृप्ति एवं सन्तोष अभीष्ट हो तो क्रियाशील रहते हुए भी हमें ज्ञानवान बनना पड़ेगा। ज्ञान का आश्रय लिए बिना, दिग्भ्रान्ति स्थिति में आशंका और उद्विग्नता ही छाई रहेगी। शान्ति तो समाधान में है, वह समाधान सद्ज्ञान का आश्रय लिए बिना अन्य किसी आधार पर हो नहीं सकती।
क्रिया स्थूल है और ज्ञान सूक्ष्म। क्रिया तक सीमित न रहकर, तत्व चिन्तन की गहराई में उतरने के प्रयत्न में, हमें चैन और सन्तोष मिलता है। एक परत इससे भी गहरी है—जिसे अन्तरात्मा कहते हैं। यहां आस्थाएं रहती हैं। अपने सम्बन्ध में, प्रिय और अप्रिय के, उचित और अनुचित के, आदतों और प्रचलनों के, पक्ष और सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अनेकानेक मान्यताएं, इसी केन्द्र में गहराई तक जड़े जमाए बैठी रहती हैं। व्यक्तित्व का समूचा ढांचा, यहीं विनिर्मित होता है। मस्तिष्क और शरीर को तो व्यर्थ ही दोष या श्रेय दिया जाता है। वे दोनों ही वफादार सेवक की तरह हर आत्मा की ड्यूटी ठीक तरह बजाते रहते हैं। उनमें अवज्ञा करने की कोई शक्ति नहीं। आस्थाएं ही प्रेरणा देती हैं और उसी पैट्रोल से धकेले जाने पर जीवन स्कूटर के दोनों पहिये—चिन्तन और कर्तृत्व सरपट दौड़ने लगते हैं। व्यक्तित्व क्या है—आस्था। मनुष्य क्या है—श्रद्धा। चेष्टाएं क्या हैं—आकांक्षा की प्रतिध्वनि। गुण, कर्म, स्वभाव अपने आप न बनते हैं न बिगड़ते हैं। आस्थाएं ही आदतें बनकर परिपक्व हो जाती हैं तो उन्हें स्वभाव कहते हैं। अभ्यासों को ही गुण कहते हैं। कर्म आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शरीर और मन को संयुक्त रूप से जो श्रम करना पड़ता है, उसी को कर्म कहते हैं। इन तथ्यों को समझ लेने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के स्तर और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले सुख-दुःखों की अनुभूति होती रही है। प्रसन्नता और उद्विग्नता को यों परिस्थितियों के उतार-चढ़ावों से जोड़ा जाता है, पर वस्तुतः वे मनःस्थिति के सुसंस्कृत और अनगढ़ होने के कारण सामान्य जीवन में नित्य ही आती रहने वाली घटनाओं से ही उत्पन्न अनुभूतियां भर होती हैं। कोई घटना न अपने आप में महत्वपूर्ण है और न महत्व हीन। यहां सब कुछ अपने ढर्रे पर लुढ़क रहा है। सर्दी-गर्मी की तरह भाव और अभाव का, जन्म-मरण और हानि-लाभ का क्रम चलता रहता है। हमारे चिन्तन का स्तर ही उनमें कभी प्रसन्नता अनुभव करता और कभी उद्विग्न हो उठता है। अनुभूतियों में परिस्थितियां नहीं, मनःस्थिति की भूमिका ही काम करती है।
जीवन के सफेद और काले पक्ष को समझ लेने के उपरान्त, सहज ही प्रश्न उठता है कि—क्या ऐसा सम्भव नहीं है कि परिस्थितियों के ढांचे में ढले—लोक-प्रवाह में बहते हुए, संग्रहीत कुसंस्कारों से प्रेरित, वर्तमान अनगढ़ जीवन को, अपनी इच्छानुसार—अपने स्तर को फिर से गढ़ा जाय और प्रस्तुत निकृष्टता को उत्कृष्टता में बदल दिया जाय? उत्तर ‘ना’ और ‘हां’ दोनों में दिया जा सकता है। ‘ना’ उस परिस्थिति में जब आन्तरिक परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा का अभाव हो और उसके लिए आवश्यक साहस जुटाने की उमंगें उठती न हों। दूसरों की कृपा सहायता के बलबूते उज्ज्वल भविष्य के सपने तो देखे जा सकते हैं, पर वे पूरे कदाचित ही कभी किसी के होते हैं। बाहरी, दैवी और संसारी सहायताएं मिलती तो हैं, पर उन्हें पाने के लिए पात्रता की अग्नि-परीक्षा में गुजरते हुए अपनी प्रामाणिकता का परिचय देना पड़ता है। उतना झंझट सिर पर उठाने का मन न हो—सहज ही कुछ इधर-उधर की ‘हथफेरी’ करके भौतिक सम्पदाएं, आत्मिक विभूतियां पाने के लिए जी ललचाता भर हो तो कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व को महामानवों के स्तर पर गठित करना और उसके फलस्वरूप उच्चस्तरीय सिद्धियां प्राप्त कर सकना एक प्रकार से असम्भव ही है। उत्तर नकारात्मक समझा जा सकता है।
‘हां’ उस स्थिति में कहा जा सकता है जबकि साधक में यह विश्वास उभरा हो कि वह अपना स्वामी आप है—अपने भाग्य का निर्माण कर सकना उसके अपने हाथ की बात है। दूसरों पर न सही अपने शरीर और मन पर तो अपना अधिकार है ही और उसके अधिकार का उपयोग करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व हस्तक्षेप कहीं से भी नहीं हो सकता। मन की दुर्बलता ही है जो ललचाती, भ्रमाती और गिरती है। तनकर खड़ा हो जाने पर भीतरी और बाहरी सभी दबाव समाप्त हो जाते हैं और अभीष्ट दिशा में निर्भयता एवं निश्चिन्तता के साथ बढ़ा जा सकता है। समुद्र की गहराई में उतरकर मोती ढूंढ़ने में विशिष्ट प्रकार के साधन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जीवन समुद्र की गहराई में उतरकर एक से एक बहुमूल्य रत्न ढूंढ़ लाना सरल है। इसमें किसी बाहरी साधना या उपकरण की जरूरत नहीं—मात्र प्रचण्ड संकल्प शक्ति चाहिए। प्रचण्ड का तात्पर्य है धैर्य और साहस का उतनी मात्रा में समन्वय जिससे संकल्प के डगमगाते रहने की बाल बुद्धि उभर आने की आशंका न हो। स्थिर बुद्धि से सतत् प्रयत्न करते रहने और फल प्राप्ति में देर होते देखकर अधीर न होने की—वरन् दूने उत्साह से प्रयत्न करने की सजीवता जहां भी होगी वहां सफलता पैर चूमने के लिए हाथ जोड़े-सिर झुकाए खड़ी होगी। ऐसे मनस्वी व्यक्ति अपने को, अपने वातावरण का यहां तक कि, अपने प्रभाव क्षेत्र को कायाकल्प की तरह बदल सकने में सफल हो सकते हैं। जीवन परिष्कार की भविष्यवाणी करते हुए ऐसे ही लोगों की सफल सम्भावना को ‘हां’ कहकर आश्वस्त किया जा सकता है।
आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए न तो सही मार्ग जानते हैं और न उस पर चलने के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा पाते हैं। दिग्भ्रान्त प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? अन्धा अन्धे को कहां पहुंचा सकता है? भटकाव में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? आज की यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्मविज्ञान का न तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और न उसका क्रिया पक्ष—साधन विधान ही निःभ्रांति है। इस उलझन में एक सत्यान्वेषी जिज्ञासु को निराशा ही लगती है।
हमें यहां अध्यात्म के मौलिक सिद्धान्तों को समझना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगढ़ तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठापित करना है, जिसके आलोक में जीवन को सच्चे अर्थों में विकसित एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसके लिए मान्यता और क्रिया क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे क्या हों, किस प्रकार हों, इस शिक्षण में थ्योरी और प्रेक्टिस के दोनों ही अवलम्बन साथ-साथ लेकर चलना होता है। थ्योरी का तात्पर्य वह है सद्ज्ञान, वह आस्था विश्वास जो जीवन को उच्चस्तरीय लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए सहमत कर सके। इसे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान और सद्ज्ञान के नामों से जाना समझा जाता है—योग इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या का तत्वदर्शन यही है। प्रेक्टिस—का तात्पर्य है वे साधन विधान जो हमारी क्रियाशीलता को दिशा देते हैं और बताते हैं कि जीवनयापन की रीति-नीति क्या होनी चाहिए और गतिविधियां किस क्रम से निर्धारित की जानी चाहिए? साधनात्मक क्रिया-कृत्यों का यह उद्देश्य समझ लिया जाय तो फिर किसी को भी न तो अनावश्यक आशा बांधनी पड़ेगी और न अवांछनीय रूप में निराश होना पड़ेगा।
यह तथ्य हजार बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि जीवन का परम श्रेयस्कर और शान्तिदायक उत्कर्ष आस्थाओं के परिष्कार—चिन्तन के निखार एवं गतिविधियों के सुधार पर निर्भर है। जीवन इन्हीं तीन धाराओं में प्रवाहित होता है। शक्ति के स्रोत इन्हीं में भरे पड़े हैं। और अद्भुत उपलब्धियां उन्हीं में से उद्भूत होती हैं। इन्हें किस आधार पर सुधारा, संभाला जाय इसकी एक विशिष्ट पद्धति है अपने अन्तरंग और बहिरंग को उच्च स्तर तक उठा ले चलना। इसे जीवन का अभिनव निर्माण एवं व्यक्तित्व का कायाकल्प भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे योगाभ्यास तपश्चर्या कहते हैं।
चेतना का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने को योग समझा जाय। क्रियाकलाप में सुव्यवस्था का आरोपण तप माना जाय। इसके लिए कई तरह के प्रयोगात्मक अभ्यास करने पड़ते हैं। पहलवान बनने के लिए अखाड़े में जाकर छोटी-छोटी कसरतों का सिलसिला शुरू करना पड़ता है। कसरतों की खिलवाड़ और दंगल में कुश्ती पछाड़ कर यशस्वी होना दो अलग स्थितियां हैं, पर दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। बीज बोने का शुभारम्भ कालान्तर में विशाल वृक्ष बनकर सामने आता है। पूजा-उपासना और स्वाध्याय मनन जैसे उपचार बीजारोपण की तरह हैं जो खाद, पानी, निराई, गुड़ाई रखवाली आदि की चिरकाल तक अपेक्षा करते हैं और समयानुसार कल्पवृक्ष बनकर मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाते हैं। आन्तरिक दृष्टि से आनन्द-विभोर और बहिरंग दृष्टि से श्रद्धा का पात्र बना हुआ भूदेव यह अनुभव करता है कि आत्म-विज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और संसार का सबसे बड़ा लाभ है।
***