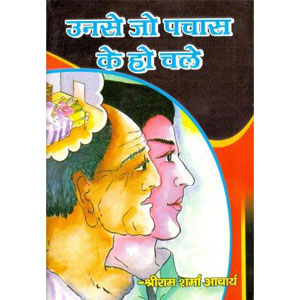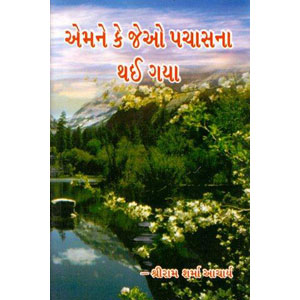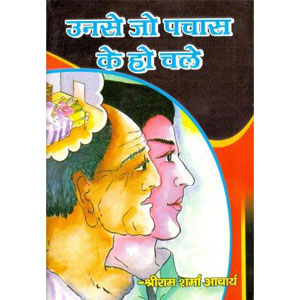उनसे जो पचास के हो चले 
वानप्रस्थ संस्कार विवेचन
Read Scan Versionजन्म और मरण की अवधि में दो बार संचय काल और दो बार उपयोग काल आता है। बालकपन और बुढ़ापा संचय काल हैं और यौवन तथा परलोक-भोग उपयोग काल हैं। संचय की अवधि में जो इकट्ठा कर लिया जाता है, उपभोग-काल में उसी का आनन्द उपलब्ध होता है बचपन में विद्याध्ययन एवं व्यायाम आदि के द्वारा जो शारीरिक, मानसिक बल उपार्जित कर लिया जाता है, उसी का सत् परिणाम यौवन काल में वैभव एवं आनन्द के रूप में उपभोग करने को मिलता है।
जिन्होंने बचपन में परिश्रमपूर्वक पढ़ाई जारी रखी, उच्च शिक्षा प्राप्त की, अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए कला-कौशल सीखी, वे अपने उस अध्ययन-तप का लाभ युवावस्था में उठाते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी-चढ़ी होने के कारण अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी, अच्छा काम मिल जाता है। अच्छी आमदनी होती है। प्रतिष्ठा का पद मिलता है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप वे शौक-मौज के, ऐश-आराम के, गौरव-सम्मान के अनेकानेक साधन जुटा लेते हैं। स्वयं मौज में रहते हैं, अपने घर वालों को मौज में रखते हैं और दूसरों का भी बहुत कुछ भला कर देते हैं।
इसी प्रकार जिनने व्यायाम, ब्रह्मचर्य, आहर-विहार के संयम द्वारा अपनी स्वास्थ्य बना लिया वे सदा निरोग रहते हैं, बहुत दिन जीते हैं, परिपुष्ट रहने से यौवन में इन्द्रिय सुख भी भोगते हैं। अच्छी नींद सोते और हंसी-खुशी के दिन बिताते हैं। पुष्ट शरीर से काम भी खूब होता है और विरोधी भी डरते रहते हैं। जो खाते हैं, पच जाता है। बीमारियों की व्यथायें नहीं सहनी पड़तीं, सन्तानें स्वस्थ होती हैं और दवा-दारू का खर्च नहीं करना पड़ता। तात्पर्य यह है कि जिसने बचपन में स्वस्थ बनने की तपश्चर्या कर ली, वह उसका लाभ जवानी में उठाता है। बचपन और कुछ नहीं, यौवन को जैसा भी कुछ बनाना हो, उसकी तैयारी का समय है। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अफसर, पहलवान आदि जो कुछ महत्व प्राप्त करना हो उसकी तैयारी का तप बचपन में ही करना होता है। जो लोग उस तैयारी की अवधि आलस्य, प्रमाद और उच्छृंखलता में बिता देते हैं, उन्हें उसका दुष्परिणाम युवावस्था में भोगना पड़ता है।
जिन लड़कों ने बचपन में पढ़ने से जी चुराया है, वे बड़े होने पर बिना पढ़े-गंवार बने रहे और आजीविका, पद तथा सामाजिक सम्मान की दृष्टि से गये-गुजरे स्तर पर पड़े रहने के लिए विवश हुए, कोई अच्छा काम न पा सके, उच्चस्तरीय लोगों के बीच सिर उठाकर बैठ सकने की स्थिति न रही। इसी प्रकार जिनने व्यायाम न किया, आहार-विहार, में असंयम बरता, ब्रह्मचर्य तोड़ा उनको जवानी आने से पूर्व ही बुढ़ापे ने धर दबाया। तरह-तरह की बीमारियों के शिकार बने रहे। देह से कुछ महत्वपूर्ण काम न हो सका। दवा-दारू में पैसा उड़ता रहा, देह कष्ट पाती रही, इन्द्रिय सुख भोगने का सौभाग्य ही न मिला, सन्तानें दुबली हुईं, अल्प अवधि में ही काल-कवलित हो गईं, जब तक जिए तब तक भी दूसरे उपहास, उपेक्षा अथवा तिरस्कार की दृष्टि से देखते और घृणा भरा व्यवहार करते रहे। बलवान शत्रुओं ने सताने में कमी न छोड़ी। अपनी दुर्बलता अपने को ही डराती एवं परेशान करती रही। बचपन में शरीर बल संचय के कर्तव्य की जो उपेक्षा की गई थी उसका दण्ड यौवन में भुगता ही जाना था, भुगतना भी पड़ा। संचयकाल की बर्बादी उपभोगकाल में विपत्ति बनकर सामने आती है, यह एक सुनिश्चित तथ्य है।
जिन्हें यौवन काल समुचित स्थिति में व्यतीत करने की महत्वाकांक्षा हो, उन्हें बचपन एवं किशोर अवस्था में उसके लिए आवश्यक तप करना ही होता है। उसके बिना और कोई रास्ता युवावस्था को शानदार बनाने का है नहीं। अपवाद की बात दूसरी है, छप्पन फाड़कर किसी को दौलत मिले तो यह उसका पूर्व संचित भाग्य ही कहा जायगा, पर आमतौर से ऐसा होता नहीं, होता यही है कि जो किया जाता है, उसका फल मिलता है। इसलिए क्या अभिभावक, क्या अध्यापक, क्या शुभचिन्तक, क्या अच्छे मित्र सभी किशोर और नवयुवकों को यही नेक सलाह देते हैं कि वे पूरी मेहनत, एकाग्रता और दिलचस्पी से अपने बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में लगे रहें। जो लउ़के इस सलाह को मान लेते हैं वे आगे चलकर सुख पाते हैं। जो इन परामर्शों पर कान नहीं धरते उन्हें समय आने पर उस उपेक्षा का बेतरह पश्चात्ताप करना पड़ता है।
दृश्य यौवन की तरह एक अदृश्य यौवन भी है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की शक्ति एवं महत्ता कहीं अधिक होती है। स्थूल शरीर की तुलना अधिक सामर्थ्यवान है। शरीर बल की तुलना में बुद्धिबल का उपयोग अधिक है। ठीक उसी प्रकार मरणोत्तर का महत्व इस दृश्य यौवन की अपेक्षा हजारों-लाखों गुना अधिक है। दीखने वाली जवानी दस-बीस वर्ष ठहरती है, पर मरने के बाद स्वर्ग-नरक की अवधि उसकी तुलना में बहुत अधिक लम्बी होती है। उसमें मिलने वाले सुख एवं दुखों का स्तर भी जवानी में मिलने वाली थोड़ी-सी सुविधा-असुविधाओं की तुलना में कहीं अधिक गहरा है। स्वर्ग में जो आनन्द है, वह सांसारिक पदार्थों में कहां? नरक में जो व्यथा-वेदना है, स्थूल जगत उसका हजारवां अंश भी नहीं। यहां तो सुख-दुख बटाने वाले भी कई मिल जाते हैं, पर वहां तो सब कुछ अकेले ही सहना पड़ता है। यौवन उसे कहते हैं जिसमें शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हों। सांसारिक जीवन में हमारी अन्तःचेतना बहुत करके प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती हैं। इन्द्रिय-लिप्सा एवं सांसारिक आकर्षण एवं मानसिक भ्रम-जंजाल उसे दबाये बैठे रहते हैं, पर मरणोत्तर काल में वे सभी हट जाते हैं और अन्तःचेतना अपने प्रौढ़ रूप में विकसित होती है। तब उसके सुख-दुख की अनुभूतियां भी तीव्र हो जाती हैं।
स्वर्ग-नरक के सुख-दुःखों का स्तर इसलिए इस संसार की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा होता है। नये जन्म की सारी भूमिका भी इसी मरणोत्तर यौवन में बन जाती है। जिस प्रकार युवावस्था में जैसा होता है वैसा ही सन्तान का भी स्वास्थ्य होता है। ठीक इसी प्रकार प्राणी को मरणोत्तर काल में जैसी संवेदनायें भुगतनी पड़ती हैं, ठीक उसी स्तर का पुनर्जन्म भी होता है। नरक भोगने वाले प्राणी संसार में उतरते हैं तो उन्हें नीच योनियों में कष्टकारक परिस्थितियों में जन्मना पड़ता है और जो स्वर्ग से आते हैं वे अपनी आत्मिक स्थिति के अनुरूप उत्कृष्ट स्तर के वातावरण में जन्मते और महत्वपूर्ण जीवन-यापन करते हैं।
उच्चस्तरीय सुख के लिए उच्चस्तरीय तप — इस मरणोत्तर जीवन को सुखी एवं समुन्नत स्तर का बनाने के लिए बुढ़ापे में तैयारी करनी पड़ती है। जिस प्रकार बचपन की सीमा रेखा से यौवन जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार बुढ़ापे की सीमा रेखा से मरणोत्तर यौवन जुड़ा हुआ है। इसलिए उस सूक्ष्म, अदृश्य किन्तु महान यौवन की तैयारी भी ठीक इन्हीं दिनों करनी पड़ती है। जिन्होंने अपनी ढलती आयु का ठीक उपयोग कर लिया, उनने मरणोत्तर यौवन को सुव्यवस्थित बनाने की योजना बना ली, किन्तु जो उस महत्वपूर्ण अवधि को आलस्य, प्रमाद और माया मोह में गंवाते रहे उनका महान मरणोत्तर यौवन उसी प्रकार अन्धकारमय बनता है जैसा कि उच्छृंखल और आवारा बच्चों का सांसारिक जीवन अस्त-व्यस्त रहता है। कितने ही बेवकूफ लड़के अपनी ढीठता में इतने ग्रसित होते हैं कि भावी जीवन के बिगड़ने की बात में उन्हें कोई सार दिखाई नहीं देता। उसी तरह कितने ही बूढ़े ऐसे अदूरदर्शी होते हैं कि वे अजर-अमर बने रहने पर विश्वास करते हैं और मरणोत्तर यौवन की समस्याओं को फूटी आंख से भी नहीं सोचना चाहते। उस सम्बन्ध में सोचने की उन्हें फुरसत ही नहीं मिलती। नाती-पोतों की ममता उन्हें छोड़ती ही नहीं। जो कमाना, जो करना, जो सोचना सो सब बेटे-पोतों के लिए ही। इस प्रकार के मूढ़ताग्रस्त बुड्ढे फिर चाहें वे पढ़े-लिखे हों या अनपढ़ सच्चे अर्थों में मूढ़मति कहे जायेंगे। आज हमारा समाज उच्छृंखल लड़कों और अदूरदर्शी मन्द मति बूढ़ों से भरा पड़ा है। फलस्वरूप हम प्राचीन गौरव गरिमा से दिन-दिन नीचे गिरते हुए पतन के गहरे गर्त में गिरते चले जा रहे हैं।
इस स्थिति को बदलना ही होगा। नव निर्माण की, युग परिवर्तन की समस्या इसी प्रकार हल होगी। बालकों में अनुशासन संयम, परिश्रम एवं शिष्टाचार की भावनाएं विकसित करके उन्हें सांसारिक प्रगति में योगदान कर सकने योग्य बनाना आवश्यक है। उसी प्रकार वयोवृद्धों को कहना होगा कि वे मरणोत्तर जीवन को समुन्नत बनाने की तैयारी में लग जायें। यह तैयारी दुहरे लाभ की है। उनका निज का परलोक स्वर्गीय सुख-शान्ति से परिपूर्ण होगा, पुनर्जन्म की महती सम्भावना रहेगी एवं मुक्ति का आनन्द मिलेगा। साथ ही इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो साधना करनी पड़ेगी, वह संसार में सर्वतोमुखी सद्भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वे करेंगे तो अपने आत्म-कल्याण का कार्य पर उसके फलस्वरूप विश्व शान्ति में जो योगदान मिलेगा वह लोक-कल्याण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जायगा। इसलिए दूरदर्शी महर्षियों ने भारतीय जीवन के अन्तिम अध्याय को जिस प्रकार व्यतीत करने की परम्परा बनाई है, उसमें दुहरा लाभ है। वृद्ध पुरुष अपना परलोक तो सुधारते ही हैं साथ ही संसार की भी इतनी बड़ी सेवा करते हैं कि इस लोक में स्वर्ग के अवतरण का मनोरम दृश्य दिखाई देने लगता है। जन साधारण को उनके इस तप से गुलाब या चन्दन की सुगन्धि की तरह अनायास ही महत्वपूर्ण लाभ मिलता है।
ढलती उम्र का तकाजा है-वानप्रस्थ — पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे ही हलकी होने लगें, घर को चलाने के लिए बड़े बच्चे समर्थ होने लगें और अपने छोटे भाई-बहिनों की देखभाल करने लगें, तब वयोवृद्ध व्यक्तियों का एक मात्र कर्तव्य यही रह जाता है कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से धीरे-धीरे हाथ खींचें और क्रमशः वह भार समर्थ लड़कों पर बढ़ाते चलें। ममता को परिवार की ओर शिथिल कर समाज की ओर विकसित करते चलें। सारा समय घर के लोगों के लिए ही खर्च न कर दें वरन् उसका कुछ अंश क्रमशः अधिक बढ़ाते हुए समाज के लिए समर्पित करते चलें।
घर छोड़कर एकान्त कुटी में जा बैठना और भजन के नाम पर निष्क्रिय जीवन बिताने लगना आजकल लोगों ने भक्ति या वैराग्य का रूप मान लिया है। इसी दृष्टि से कई अध्यात्मवादी व्यक्ति तीर्थों में, नदियों के किनारे एकान्त कोठरियों में जा बैठने को ही बड़ा आध्यात्मिक पुरुषार्थ मान बैठते हैं, यह धारणा अज्ञानान्धकार युग के निराशावादी और अकर्मण्य लोगों ने फैलाई जिसके फलस्वरूप आज 80 लाख व्यक्ति धर्म के नाम पर निष्क्रिय, अनुपयोगी जीवन बिताते हुए भिक्षुक बने हुए जनता पर भार बनकर जी रहे हैं। यह विडम्बना न अध्यात्म है, न धर्म, न योग है, न वैराग्य। न उससे व्यक्ति का भला होता है और न समाज का। प्राचीनकाल का वैराग्य रचनात्मक वैराग्य था, जिसमें व्यक्ति के कल्याण तथा समाज के उत्कर्ष का उभय पक्षीय कार्यक्रम समान रूप से सन्निहित थे। बुढ़ापे को वानप्रस्थ के लिए समर्पित करने का जो शास्त्रीय विधान है। उसका स्वरूप यह है कि (1) उपासना (2) स्वाध्याय, (3) संयम, (4) सेवा, इन चार कार्यक्रमों में अपनी शक्तियों को सुव्यवस्थित रीति से संलग्न किया जाय। वृद्धों को उचित है कि घर-परिवार से अपना समय और मन जिस अनुपात में बचावें, उसे उसी अनुपात से इन चार कार्यों में संलग्न करते चलें।
वानप्रस्थ का अर्थ घर छोड़कर किसी दूर देश में चले जाना कदापि नहीं। घर से सम्पर्क शिथिल हो, पारिवारिक ममता घटे, इस दृष्टि से घर में एक अलग कमरा लेकर रहने लगना और यह सोचना कि मैं छात्रावास निरीक्षक की तरह इस परिवार का मार्गदर्शक तो हूं, पर इनसे बंधा हुआ नहीं, वरन् मेरा जीवन समाज की सम्पत्ति है, वास्तविक वानप्रस्थ है। जहां तक सम्भव हो, परिवार की स्थिति यदि उपयुक्त है तो निर्वाह खर्च घर से ही लेना चाहिए। जिनकी पेन्शन है या जिनकी पूर्व संचित सम्पत्ति, कृषि आदि है वे उसका उपयोग अपने निर्वाह में भी करें तो यह न्यायोचित है। यह जरूरी नहीं कि अपनी उपार्जित अब तक की सारी सम्पदा परिवार को ही दे दी जाय और खुद भिक्षुक बनकर दूसरों की रोटी पर जिया जाय। आजकल दूसरों को धान्य कुधान्य ही है। उसे खाने से आत्मिक विकास में सहायता नहीं मिलती वरन् बाधा ही पड़ती है। इसलिए सेवा कार्य में संलग्न स्थिति में कहीं अवसर आने पर किसी के यहां रोटी खाली यह बात दूसरी है, साधारणतया गुजारा अपने बलबूते पर ही करना चाहिए। यदि पारिवारिक स्थिति ठीक न हो तो कुछ समय परिश्रम करके गुजारे की व्यवस्था निकाल ले और बाकी समय अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों में लगावें।
कार्य पद्धति की रूपरेखा — किसी जमाने में वानप्रस्थ लोग वनों में रहते थे। उस जमाने में वनों में कन्दमूल फल इतने अधिक थे कि जीवन निर्वाह की व्यवस्था गांव, नगरों की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से हो जाती थी। अब कहीं ऐसा जंगल नहीं रहा, इसलिए निर्वाह की सुविधा गांव-नगरों के माध्यम से ही जुटानी पड़ती है। अतएव निवास का प्रबन्ध भी वैसा ही करना उचित है। प्राचीनकाल में वानप्रस्थी पीत वस्त्र धारण करके ऋषियों के गुरुकुलों में छात्रों की तरह ही स्वाध्याय करते थे। बच्चों की पढ़ाई में और बूढ़ों की पढ़ाई में अन्तर तो होता है, पर रीति एक ही है। वानप्रस्थों को अपना मानसिक विकास करने के लिए स्वाध्याय की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। प्राचीनकाल में वानप्रस्थ संयम की दृष्टि से ब्रह्मचर्य और आहार के सम्बन्ध में पूरी कड़ाई बरतते थे। आज की परिस्थिति में इतनी ढील रखी जा सकती है कि इंद्रियों का संयम अधिकाधिक सावधानी से किया जाय, पर ऐसा कोई व्रत न लिया जाय जो टूट जाय तो आत्मग्लानि में जलना पड़े। उपासना का द्वार गृहस्थ और विरक्त सबके लिए समान रूप से खुला है। गृहस्थी की उपासना बहुत थोड़ी चल पाती है और अनियमित भी हो जाती है, वानप्रस्थ इस सम्बन्ध में अधिक तत्परता बरतें। उनकी साधना संकल्पपूर्वक, नियमित एवं व्यवस्थित चलनी चाहिए। समय भी अपेक्षाकृत अधिक लगाना चाहिए, चौथा काम सेवा का है। वयोवृद्ध वानप्रस्थों को जनमानस का स्तर ऊंचा उठाने, जनता में सद्भावना एवं सत्प्रवृत्तियां उत्पन्न करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप रचनात्मक कार्यक्रम बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए उसी उत्साह से लगा रहना चाहिए जैसे कि गृहस्थ में धन उपार्जन के लिए तत्परता बरती जाती है। वानप्रस्थ का प्रतीक पीत वस्त्र है। सारे वस्त्र पीले न हों तो एक दुपट्टा या रूमाल पीले रंग का अपने पास एक धार्मिक वर्दी की तरह रखा जा सकता है। उपर्युक्त क्रम में यदि अपना जीवन क्रम ढाल लिया जाय तो समझना चाहिए कि वानप्रस्थ की तैयारी एवं व्यवस्था पूर्ण हो गई।
उपर्युक्त प्रकार की सुविधा जो जुटा सकते हैं, उन्हें पचास वर्ष की आयु के बाद भी वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। जिनके पास पहिले से ही पारिवारिक गुजारे की व्यवस्था बनाने के लिए पैतृक सम्पत्ति मौजूद है, या जिनके बाल-बच्चे हैं ही नहीं वे किसी भी आयु में वानप्रस्थ ले सकते हैं। उन्हें एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि वानप्रस्थ के उपरान्त सन्तानोत्पादन न करें।
आश्रम वानप्रस्थ संस्कार भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण है। जीवन को ठीक प्रकार जीने की समस्या उसी से हल होती है। युवावस्था के कुसंस्कारों का शमन एवं प्रायश्चित इसी साधना द्वारा होता है। जिस देश, धर्म, जाति तथा समाज में उत्पन्न हुए हैं, उनकी सेवा करने का, ऋण-मुक्त होने का अवसर भी इसी स्थिति में मिलता है। इसलिए जिन भी नर-नारियों की स्थिति इसके लिए उपयुक्त हो उन्हें वानप्रस्थ लेना चाहिए। एक प्रतिज्ञा बन्धन में बंध जाने पर व्यक्ति अपने जीवन क्रम को तदनुरूप ढालने में अधिक सफल होता है। बिना संस्कार कराये मनोभूमि पर वैसी छाप गहराई तक नहीं पड़ती। इसलिए कदम कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते रहते हैं। विवाह न होने तक प्रेमिका का सहचरत्व संदिग्ध रहता है, पर जब विवाह हो गया तो सब कुछ स्थाई एवं सुनिश्चित हो जाता है। संस्कार के बिना पारमार्थिक भावनाओं का उफान कभी शिथिल या समाप्त भी हो सकता है, पर यदि विधिवत् संस्कार कराया गया तो अन्तःप्रेरणा तथा लोक-लज्जा दोनों ही निर्धारित गति-विधि अपनाये रहने की प्रेरणा देती रहेंगी। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुरूप जिन्हें सुविधा हो वे विधिवत् संस्कार करा लें। जिन्हें सुविधा न हो वे बिना संस्कार के भी उपर्युक्त प्रकार की रीति-नीति अपनाने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न करते रहें।
सुसंस्कार का सृजन — वृद्धावस्था में जो संस्कार जमते हैं वे ही मरणोत्तर जीवन में साथ जाते हैं, इसलिए इस अवधि में उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरे रहने और उत्कृष्ट गतिविधियां अपनाये रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार और कर्म दोनों के सम्मिलन से ही संस्कार बनते हैं और यह संस्कार ही प्राणी के साथ जाते हैं। विचारों की उत्कृष्टता अर्जित करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय नितान्त आवश्यक है। इस अध्ययन की पुष्टि तब होती है, जब उसे दूसरों को भी सुनाया जाय। जिस प्रकार पढ़ने और लिखने की दोनों क्रियायें मिलने पर पढ़ाई का पूरा क्रम बनता है, केवल पढ़ते ही रहें लिखें नहीं तो साक्षरता अधूरी रहेगी। इसी प्रकार स्वाध्याय तो करें पर उसे किसी को सुनावें नहीं तो वह अध्ययन भी ठीक तरह हृदयंगम नहीं हो सकेगा। ज्ञान अर्जन और ज्ञान दान दोनों ही वानप्रस्थी के आवश्यक कर्तव्य हैं। उपासना भी उसी प्रकार उभय पक्षीय है। भगवान का भजन, ध्यान, पूजन, जप, कीर्तन एक पक्ष है, दूसरा पक्ष विश्व मानव के, विराट् ब्रह्म के इस मूर्तिमान स्वरूप संसार की रचनात्मक सेवा करने से, विचार और कार्य का समन्वय होने से भजन में समग्रता आती है। जो केवल माला फेरते हैं, सेवा से कतराते हैं, उनका भजन वैसा ही है जैसा कि रोटी तो खाना पर पानी न पीना। आहार-विहार का संयम शारीरिक, मानसिक स्वस्थता की दृष्टि से आवश्यक है। इन्द्रिय निग्रह की तपश्चर्या से मनुष्य की भावनात्मक प्रवृत्तियों का मोड़ वासना, तृष्णा से हटकर परमार्थ प्रयोजनों की ओर प्रवाहित होता है। यह सारी विधि-व्यवस्था ऐसी है जिससे वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी अन्तःचेतना को उस मार्ग पर विकसित करते हैं जिस पर चलते हुए मरणोत्तर यौवन में अक्षय सुख-शान्ति को प्राप्त कर सकना सरल हो जाता है।
लोक शिक्षण की आवश्यकता — इस गतिविधि के अपनाने से समाज की भी भारी सेवा होती है। प्राचीनकाल में लोक निर्माण की सारी गतिविधियां एवं प्रवृत्तियों के संचालन का उत्तरदायित्व साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थों पर ही था। वे अपनी सारी शक्तियां परमार्थ भावना से प्रेरित होकर जन साधारण को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किए रहने में लगाये रहते थे। फलस्वरूप चारों ओर धर्म, कर्तव्य, सदाचार का वातावरण ही बना रहता था। वयोवृद्ध, अनुभवी, परमार्थ परायण लोक सेवियों का प्रभाव जन-साधारण पर स्वभावतः बहुत गहरा पड़ता है। टिकाऊ भी होता है। ऐसे लोग जन नेतृत्व करने के लिए जब धर्मतंत्र का उचित उपयोग करते थे तो सारे समाज में सत्प्रवृत्तियों के लिए उत्साह उमड़ पड़ता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, न्याय, विवेक, वैभव, शासन, सुरक्षा, व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में यह वयोवृद्ध लोग ही नेतृत्व करते थे। इतने अधिक अनुभवी और धर्म परायण व्यक्तियों की निःशुल्क सेवा जिस देश या समाज को उपलब्ध होती हो उसको संसार का मुकुटमणि होना ही चाहिए। प्राचीन काल में ऐसी ही स्थिति थी। आज वानप्रस्थ की परम्परा नष्ट हुई, बूढ़े लोगों को लोभ, मोह के बन्धनों में ही ग्रसित रहना प्रिय लगा तो फिर देश का पतन अवश्यंभावी था, हुआ भी, हो भी रहा है।
यह पुण्य परम्परा पुनः सजीव हो — प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि समाज में पूर्वकाल की भांति यह प्रथा प्रचलित हो कि हर ढलती आयु का व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर पारमार्थिक जीवन जिए और समाज द्वारा विविध-विध प्राप्त हुईं सुख-सुविधाओं का ऋण वृद्धावस्था में समाज सेवा का व्रत लेकर चुकाये। अपना परलोक सुधारे, जीवन सार्थक करे और संसार को सुरम्य बनाने में समुचित योगदान करे।
मूल प्रयोजन समझा जाय — वानप्रस्थ का मूल प्रयोजन अपनी आत्मीयता एवं ममता को छोटे से परिवार तक सीमित न रखकर विश्व-मानव तक विस्तृत एवं विकसित कर देना है। आत्मोन्नति इसी को कहते हैं। आत्मा तो सीढ़ियों पर चढ़ती है और न उसकी धन, वजन, पद आदि की दृष्टि से उन्नति होती है। जितने छोटे दायरे में पहले अपनेपन का भाव सीमित था, वह यदि बढ़ता है, विस्तृत होता है, अनेकों परिवार अपने ही परिवार दीखते हैं और अनेकों व्यक्ति अपने ही कुटुम्बी लगते हैं, तो समझना चाहिए कि आत्मा की, उसके दृष्टिकोण एवं सद्भाव की वृद्धि हुई है। यही प्रगति आत्मा को परमात्मा एवं नर को नारायण बनाती है। जब तक मनुष्य अपने शरीर एवं परिवार को ही अपना मानेगा तथा अन्य शरीरों के प्रति परायेपन का भाव रखेगा तक तक वह बन्धनों में बंधा हुआ ही कहा जायगा। स्वार्थपरता के बन्धन जैसे-जैसे ढीले होते जाते हैं, परमार्थ में स्वार्थ दिखाई देता है, बिराने, अपने जैसे लगते हैं और अपनों के प्रति जो ममता होती है, वह विस्तृत होकर सर्वसाधारण के लिए व्यापक हो जाती है। तब यह समझा जाता है कि आत्मा अपनी लघुता छोड़कर महान् बनने के लिए अणु से विभु और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए अग्रसर हो रही है। भजन करने का उद्देश्य इसी स्थिति को प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक व्यायाम करना है। यह लघुता जैसे-जैसे महानता में, स्वार्थपरता ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम्’’ स्तर में विकसित होती जाती है, वैसे ही वैसे ईश्वर अपने निकट आता जाता है। जिस दिन सबमें अपनी ही आत्मा प्रकाशवान् दिखाई पड़े तो कहते हैं कि शारीरिक साक्षात्कार हो गया। इसी प्रकार यदि अपनेपन का भाव अन्य शरीर रूपी दर्पणों में दीख पड़े तो समझना चाहिए आत्म-साक्षात्कार होने लगा। स्वप्न में किसी देवता की प्रतिमा दीख पड़ना या जाग्रत अवस्था में ध्यान, एकाग्रता से कोई उपासना प्रतीक चलते-फिरते नजर आ जाना, यह तो अपनी कल्पना की सघनता अथवा भावना की एकाग्रता का छोटा-सा चमत्कार मात्र है। ऐसे भाव दर्शन तो उन प्रियजनों के भी होते रहते हैं जिनके प्रति अपना आकर्षण अधिक होता है। इनका अधिक मूल्य या महत्व नहीं। इस प्रकार का अनुभव यदि किसी को होने लगे तो उससे यह मान्यता न बना लेनी चाहिए कि हमें ईश्वर-दर्शन हो गये या भगवान की अनुकम्पा प्राप्त हो गई। वास्तविक आत्म–साक्षात्कार तो प्राणिमात्र में ईश्वर की सत्ता समाई हुई देखकर, उनके प्रति सद्व्यवहार करने की भावना का उदय होने को ही कहते हैं। कल्याण तो उसी स्थिति में पहुंचने वाले का ही होता है।
योगाभ्यास एवं तपश्चर्या — वानप्रस्थ में इसी आत्म-विस्तार का योगाभ्यास करना पड़ता है। यह सब कहने-सुनने में तो सरल है, पर करने में कठिन है। जब तक कोई मान्यता व्यवहार रूप में न उतरे तब तक मान्यता का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रत्यक्ष आराधना, उपासना, सेवा-धर्म अपनाये बिना नहीं हो सकती। इसलिए वानप्रस्थ में नर-नारायण की सेवा के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाना पड़ता है और अपने अधिकांश समय, श्रम, धन एवं मनोयोग इसी प्रयोजन के लिए समर्पित करने होते हैं। यह कर्म-पद्धति विशुद्ध रूप से योग साधना एवं तपश्चर्या है। धूप में या पानी में खड़े रहने की अपेक्षा जन-सेवा की साधना अधिक उपयुक्त है क्योंकि उससे दूसरों को लाभ पहुंचता है और अपने को तत्काल सन्तोष मिलता है। धूप में खड़े रहने से उन दोनों में से एक भी प्रयोजन नहीं सधता, न किसी को लाभ पहुंचता है और न अपने अन्तःकरण में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने जैसा सन्तोष ही अनुभव होता है।
ईश्वर उपासना एवं भजन — वह भजन भी करता है और भक्ति भी। प्रातः-सायं श्रद्धापूर्वक प्रभु का नाम स्मरण करता है-गायत्री मन्त्र जपता है, हृदय खोलकर प्रभु के सामने रखता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं गुण-कर्म-स्वभाव में उत्कृष्टता बढ़ाने की प्रार्थना करता है, सत्पथ पर चलने में आने वाली कठिनाइयों से जूझ सकने लायक आत्मबल एवं साहस की याचना करता है। भाव-विभोर होकर की हुई ऐसी प्रार्थना भी ईश्वर के अन्तःस्थल पर चोट करती है। ऐसे सच्चे सदुद्देश्य के लिए, न्याय और नीति की मर्यादायें सुरक्षित रखने वाली प्रार्थना सुनकर ईश्वर द्रवित हो उठता है और वह उस ज्ञानी भक्त के ऊपर अपने प्यार की, अनुग्रह की, अविरल वर्षा करने लगता है।
ऐसे ईश्वर-भक्त वानप्रस्थ के लिए यह आवश्यक नहीं कि पूरा दिन माला घुमाने में ही लगा दे। महात्मा गांधी की तरह वह एक घण्टे भी सच्चे मन से निकली हुई, ईश्वर की अंतरात्मा को छूने वाली पुकार-प्रार्थना करता रहे, तो वह चौबीस घण्टे आंख बन्द किए ध्यान-भजन करते रहने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। धर्म युद्ध के मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक यदि अपना गोला-बारूद चलाते हुए दो-पांच मिनट भी ईश्वर का नाम ले लिया करें तो वे उनका पूरा सन्ध्या-वन्दन हो जाता है। वह कथा प्रसिद्ध है जिसके अनुसार एक देवदूत की बगल में भक्तों की नामावली देखकर किसी लोकसेवी ने इसमें अपना नाम होने न होने की जिज्ञासा की थी। नाम न निकला तो दुःखी भी हुआ था, जप जब दूसरा देवदूत आया और उसकी बगल में लगी छोटी पुस्तक के बारे में लोकसेवी ने पूछ-ताछ की तो देवदूत ने बताया कि उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनका भजन ईश्वर स्वयं करते हैं और उस पुस्तक में सबसे पहले इस लोकसेवी का नाम था।
कथा चाहे अलंकारिक ही क्यों न हो पर उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता का नग्न उद्घाटन किया गया है। एक महान सचाई को ज्यों की त्यों खोलकर रख दिया गया है। अध्यात्मवाद का सार यही है। भजन शब्द ‘भज्’ धातु से बना है जिसका अर्थ ‘सेवा’ ही होता है। कहते भी हैं ‘पूजा-सेवा’ करते हैं। पूजा, सेवा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जिस विधान में सेवा सम्मिलित नहीं वह न तो पूजा है न आराधना। सेवा की गंगा में स्नान किए बिना किसी की आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। जो ईश्वर का अनुग्रह चाहता है, उसे ईश्वर के पुत्रों पर अनुग्रह करना होता है। जो मनुष्य रूपी खेतों में दया के बीज बोता है, उसे ही ईश्वर की छाया प्राप्त करने का प्रतिफल उपलब्ध होता है। जनता-जनार्दन की, नर-नारायण की, पुरुष-पुरुषोत्तम की भक्ति करने के लिए सेवा-धर्म को जीवन में ओत-प्रोत करना होता है और यही वह तपश्चर्या है जिसके आधार पर वानप्रस्थ को या किसी को भी प्रभु का वास्तविक अनुग्रह प्राप्त कर सकना संभव होता है।
स्वेद एवं स्नेह का अभिसिंचन — वानप्रस्थ की उपासना पद्धति लोक-सेवा के साथ जुड़ी रहती है। यह प्रातः-सायं आवश्यक पूजा-भजन करता रहता है, साथ ही दिन-रात अपने चारों ओर ईश्वर की चलती-फिरती प्रतिमाओं को अपने स्वेद एवं स्नेह से सिंचित करने का भी ध्यान रखे रहता है। इस भावना से प्रेरित होकर वह अपनी योग्यता और निकटवर्ती परिस्थितियों का तालमेल बिठाकर इस प्रकार के कार्यक्रम बनाता रहता है, जिसके आधार पर समीपवर्ती लोगों का आन्तरिक स्तर ऊंचा उठे, विवेक जागे, सत्प्रवृत्तियों का उदय हो और गुण, कर्म, स्वभाव में परिष्कार आरम्भ हो। मनुष्य का आन्तरिक स्तर ऊंचा उठाना, यही तो उस पर अमृत वर्षा करना है। जिस आत्मा का बुझा हुआ प्रकाश चमक उठा, समझना चाहिए कि उसके लिए सभी विभूतियों को प्राप्त करने का द्वार खुल गया। मनुष्य अपनी कुपात्रता के फलस्वरूप ही अवनति के गर्त में पड़ा नरक भोगता रहता है। जब उसकी पात्रता प्रखर होती है, तो वह गई-गुजरी परिस्थितियों को तोड़-मरोड़ कर रख देता है और हर हालत में अपने लिए स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, जिसने अपनी गतिविधियों के निर्माण की कला सीख ली उसके भाग्योदय में देर ही कितनी लगती है। इन तथ्यों की वास्तविकता को समझते हुए वानप्रस्थ के सेवा कार्य-क्रमों का क्रम उसी प्रकार बनता है जिससे समीपवर्ती लोग सद्विचारों एवं सत्कर्मों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। इससे बढ़कर मनुष्य की और कुछ सेवा हो भी नहीं सकती। अन्न, वस्त्र, धन आदि देने से किसी की क्षणिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और कुछ समय बाद वही अभाव फिर सामने आ उपस्थित होता है, पर जिसका अन्तःकरण, मानसिक स्तर एवं चरित्र ऊंचा उठा दिया गया, वह तेजी से आगे बढ़ता है, अपना उद्धार करता है और दूसरे अनेकों के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम करता है।
जो कार्य-पद्धति साधु-ब्राह्मणों की सदा से रही है उसी को वानप्रस्थी अपनाते हैं। जन-जागरण, विवेक का परिष्कार, चरित्रगठन, सद्भाव-अभिवर्धन, कर्तव्य-पालन, सहृदयता एवं सेवा भावना का उन्नयन जिन भी कार्यों के द्वारा सम्भव हो सके, उनका आयोजन करते रहना ही उसे अभीष्ट होता है। चूंकि इस प्रकार की प्रवृत्तियां धार्मिक वातावरण में ही पनपती और परिपुष्ट होती हैं इसलिए उसे ऐसे धार्मिक कर्मकाण्डों, विधि-विधानों, आयोजनों, उत्सवों एवं रचनात्मक क्रम-विधानों की भी व्यवस्था करनी होती है, जिससे धर्म-शिक्षा के उपयुक्त वातावरण विनिर्मित हो सके। स्वाध्याय एवं सत्संग का, शिक्षा एवं विद्या का कोई न कोई विधि-विधान उसे रचते ही रहना पड़ता है। जनसम्पर्क के लिए सम्मान एवं संकोच को छोड़कर घर-घर अलख जगाता फिरता है। जन-जन के पास जाता है, कोई उसकी उपेक्षा करता है या उपहास करता है तो भी विचलित नहीं होता, वरन् ऊसर में खेती करने वाले साहसी किसान की तरह दिन, रात चौगुने उत्साह के साथ अपने प्रयत्नों को जारी ही रखे रहता है।
शतसूत्री साधना क्रम — युग निर्माण योजना के अन्तर्गत शतसूत्री कार्यक्रमों की सुविस्तृत शृंखला इसी उद्देश्य से बनाई गई है। आज की परिस्थितियों में जिन सर्वांगीण सुधार-सेवाओं की आवश्यकता है, उन्हें इस शतसूत्री योजना में जोड़ दिया गया है। साधु-ब्राह्मणों और वानप्रस्थों को इनमें से जो भी कुछ जहां जिस प्रकार करना उपयुक्त लगे, वहां-वहां आरम्भ किया जा सकता है। कार्यक्रमों का बाह्य माध्यम कुछ भी क्यों न हो, उसके मूल में व्यक्ति के अन्तःकरण का विकास ही सन्निहित रहना चाहिए। भौतिक उन्नति की योजनाओं में दूसरे लोग लगे हैं, वह राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों का काम है। उनमें हमें नहीं उलझना चाहिए। धार्मिक लोगों का सेवा-क्षेत्र विशुद्ध रूप से भावनात्मक होना चाहिए। यह इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि उसे यदि धर्मक्षेत्र के लोग पूरा कर सकें तो मानव जाति की अगणित समस्याओं में से 99 प्रतिशत का हल हो सकता है। भौतिक लाभ बढ़ जाय किन्तु आन्तरिक स्तर गिरा रहे तो मनुष्य का कुछ भी भला न होगा किन्तु यदि आत्मिक स्तर उठ जाय तो भौतिक स्तर गिरा हुआ रह ही नहीं सकता, यदि रहे भी तो उससे कुछ बिगड़ नहीं सकता। अतएव जन-मानस में सद्भावनाओं की, सत्प्रवृत्तियों की कृषि करना और उसे सुरभित फलते-फूलते उद्यान के रूप में बनाये रहना, यही साधु पुरुषों का काम होता है। चतुर माली की तरह वे धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं सुसंस्कारिता की वाटिका को सुरम्य बनाने में एक कर्मठ माली की तरह लगे रहते हैं। इस साधना एवं तपश्चर्या में लगा हुआ उनका प्रत्येक स्वेद-बिन्दु प्रत्येक भाव-कण उनके स्वयं के लिए ही नहीं समस्त संसार के लिए वरदान बनकर सामने आता है, उससे विश्व-शान्ति की वास्तविक सम्भावना का सृजन होता है।
जिनके जीवन का पूर्वार्द्ध बीतने की सीमा तक पहुंचा हो, उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या शेष जीवन भी इसी तरह गुजारना है जैसा कि आम लोग गुजारते हैं? मनुष्य जीवन की महत्ता एवं उसके अनुपम सौभाग्य का मूल्य-महत्व हमें समझना चाहिए और इस अलभ्य अवसर को ऐसे ही अर्द्धतंद्रित अवस्था में बिता नहीं देना चाहिए। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ करना ही चाहिए, जिनके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। समाज का वह ऋण चुकाना ही चाहिए जिसका लाभ हम तथा हमारे परिवार उठा रहे हैं। पत्नी की वैसी स्थिति न हो तो उसका कर्ज भी हम चुकावें, क्योंकि वह आत्म-समर्पण करने के बाद अपने को लय कर चुकी तो उसकी जिम्मेदारी भी अपने ही ऊपर आ गई। माता-पिता कर्ज छोड़ करते हैं तो वह भी बेटे को चुकाना पड़ता है। यदि हमारे माता-पिता कोई अभिनव आदर्श अपने पीछे नहीं छोड़ गये हैं, या बिना समाज का ऋण चुकाये ही रह गये हैं, तो वह भी हमें चुकाना चाहिए। वानप्रस्थ व्रत लेकर अपने को और अपने परिवार को एक नैतिक ऋण से मुक्त करना चाहिए। सेवा धर्म अपनाये बिना जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। इसलिए विचारशीलता एवं दूरदर्शिता का आश्रय लेकर हमें यही निश्चय करना चाहिए कि जीवन का उत्तरार्द्ध पारमार्थिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया जाय।
जन्म–जन्मान्तर की यातना सहकर आज जो हमने यह मानव जीवन पाया है, इस जीवन का सदुपयोग कर परमात्म सत्ता का ज्ञान प्राप्त करें। हम जान लें कि हम उसी परमात्म सत्ता के अंश हैं। यह बड़ी मूर्खता होगी कि हम अपने उस सत्य स्वरूप को पाने का प्रयत्न न कर पुनः असंख्यों अधम योनियों में भटकने के लिए वापस चले जायें, इसे पागलपन के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। जो जिन कक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका है और उन्हीं में वापस जाने की सोचे। उच्च पद पर से पतित हो जाने से बढ़कर जीवन की असफलता और क्या हो सकती है? पर यदि हम परमात्मा को पाने के लिए उसके उपाय में समय रहते नहीं लगते तो इस अमूल्य मानव जीवन की निस्सारता एवं असफलता की आशंका बनी ही रहेगी। अतः उस उच्च स्थिति को पाने तक हमारा पावन कर्तव्य है कि हम ईश्वर प्राप्ति को शेष जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बनाकर तदनुरूप जीवन व्यतीत करें। स्मरण रखिए जिसको जीवन के सदुपयोग की चिन्ता हो गई, जिसने सत्य का, धर्म का तथा पवित्रता का अवलम्बन ग्रहण कर लिया उसे अपने अन्दर आत्म–सन्तोष और बाहर से सहयोग एवं सम्मान की तरंगें उठती दिखाई देंगी और वह परमानन्द में निमग्न होकर मानव जीवन भर की सफलता का रसास्वादन कर रहा होगा। ईश्वर ने हमें इस कर्मक्षेत्र में मुख्यतः भेजा ही इसीलिए है कि हम सत्कर्म और सात्विकी साधना तथा उपासना करके दैवी मार्ग पर अग्रसर हों और जीवन को उच्चतर बनाते हुए अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करें अतः श्रद्धा, लगन व दृढ़ आत्म-विश्वास के साथ अपने इस शेष जीवन को लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त उत्सर्ग करने में नियोजित कीजिए।
***
*समाप्त*