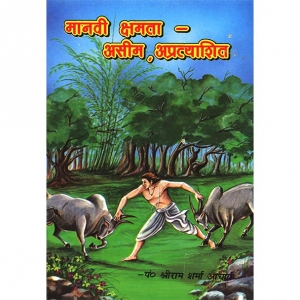मानवी क्षमता असीम अप्रत्यासित 
पहले मन को संस्कारित कीजिए
Read Scan Version
मन की दो सर्वज्ञात विशेषताएं हैं—चंचलता एवं सुख लिप्सा। बन्दर जैसी उछल-कूद, आवारा छोकरों जैसी मटरगश्ती, चिड़ियों की तरह यहां-वहां फुदकते फिरना, उसकी चपलवृत्ति को संतुष्टि पहुंचाते हैं। कल्पना के महलों की सृष्टि, कल्पना लोकों का तीव्र भ्रमण-विचारणा, उसकी शक्ति का बड़ा अंश तो इन्हीं भटकनों, जंजालों में नष्ट हो जाते हैं। शक्ति का यह व्यर्थ छीजन रोककर उसे सुनिश्चित एवं सार्थक प्रयोजन में केन्द्रित करना ही योगाभ्यास है। शक्तियों का यह सही उपयोग जीवन में स्पष्ट और आश्चर्यजनक परिणाम सामने लाता है। पिछड़ेपन के स्थान पर प्रगतिशीलता आ जाती है। दरिद्रता समृद्धि में परिणत हो जाती है। भटकाव की जगह प्रचण्ड पुरुषार्थ प्रवृत्ति पनपने पर परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती हैं और साधन संचित होने लगते हैं। लौकिक सफलताएं भी लक्ष्य केन्द्रित पुरुषार्थ का ही परिणाम होती हैं। मन की भटकन रोककर ही उसे लक्ष्योन्मुख बनाया जा सकता है।
यही सधा हुआ मन आत्मिक क्षेत्र में लगाये जाने पर सुषुप्त शक्ति केन्द्रों को जागृत व क्रियाशील बनाता है और दिव्य क्षमताएं प्रकाश में आती हैं। अन्तश्चेतना का परिष्कार सामान्य व्यक्ति को महामानव स्तर पर ले जाकर ही रहता है। प्रगति का सम्पूर्ण इतिहास मनःशक्ति के पुंजीभूत, लक्ष्य केन्द्रित पुरुषार्थ की ही यश गाथा है। चंचलता का प्रकृति को पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में परिवर्तित करने का पराक्रम ही प्रगति का सार्वभौम आधार रहा है।
मन की दूसरी प्रवृत्ति है—सुख लिप्सा। शारीरिक सुखों के भोग का माध्यम है—इन्द्रियां। उनके द्वारा विभिन्न वासनाओं का स्वाद मिलता है। पेट और प्रजनन से सम्बन्धित सुखों के लिए तरह-तरह की चेष्टाओं में ही मल उलझा रहता है और इन सुखों की प्रापित के लिए प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि इनकी मात्र कल्पनाएं करने में भी बहुत अधिक समय नष्ट करता है। फिर इन भौतिक सुखों के लिए साधन जुटाने में भी मन को जाने कितने ताने-बाने बुनने पड़ते हैं। इन्द्रियों की प्रिय वस्तु या व्यक्ति देखने, सुनने, छूने, सूंघने अथवा स्वाद लेने की लिप्साएं मन को ललक से भर देती हैं और वह उसी दिशा में लगा रहता है। अहंकार की पूर्ति के लिए मन औरों पर प्रभाव डालने हेतु तरह तरह की चेष्टाएं करता है और व्यक्ति भांति-भांति ठाट-बाट बनाता है। संग्रह और स्वामित्व की इच्छाएं भी अनेक विधि प्रयत्नों का कारण बनती हैं। इन सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं की प्यास को व्यक्त करने के लिए ही तृष्णा शब्द का प्रयोग होता है। अहं-भावना पर आघात पहुंचते ही प्रतिशोध की उत्तेजना प्रबल हो उठती है। इच्छित विषय पर अपना हक मान लेना और फिर उसके न प्राप्त होने या प्राप्ति में बाधा पड़ने पर भड़क उठना भी, अहंता पर आघात के ही कारण होता है। यह उत्तेजना ही क्रोध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि सम्पूर्ण विकार-समूह वस्तुतः मन में उठने वाली प्रतिक्रियाएं मात्र हैं, जो भौतिक सुख की लिप्साओं के कारण उठती रहती हैं। लिप्सा की इस ललक की दिशा को उलट देना ही तप है। वह दूसरी दिशा भौतिक सुखों की वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति से होने वाले क्षणिक सुखों को नहीं है। वरन् आनन्द की है। आनन्द उपभोग से नहीं, उत्कर्ष और उत्सर्ग से प्राप्त होता है। सुख मन का विषय है, जब कि आनन्द और आत्म-सन्तोष आत्मा का। सुख लिप्सा का अभ्यस्त मन आनन्द के अस्वाद को नहीं जान पाता और जिसे जाना ही नहीं, उसके प्रति गहरी स्थायी प्रीति, सच्चा आकर्षण सम्भव नहीं। आनन्द की आकांक्षा विषय-लोलुप मन में प्रगाढ़ नहीं होती। उसके लिए तो मन का प्रशिक्षण आवश्यक है। यह प्रशिक्षण—प्रक्रिया ही तप है। तपस्वी को कष्ट इसी अर्थ में सहना पड़ता है, कि अभ्यस्त सुख का अवसर जाता रहता है। शारीरिक सुख-सुविधाएं सिमटती हैं, मानसिक आमोद-प्रमोद का भी अवकाश नहीं रहता और आदर्श-निष्ठ आचरण आर्थिक समृद्धि के भी आड़े ही आता है। प्रत्यक्ष तौर पर तो, ऐसे परिणामों के लिए किया जाने वाला प्रयास मूर्खता ही प्रतीत होगा।
लेकिन श्रेष्ठ उपलब्धियों का राज-मार्ग यही है किसान, विद्यार्थी, पहलवान, श्रमिक, व्यवसायी, कलाकार आदि को भी अपनी प्रगति की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए बाल-चंचलता से मन को विरत ही करना पड़ता है और अपने नीरस प्रयोजनों में ही मनःशक्ति नियोजित करनी पड़ती है। शौक-मौज के अभ्यस्त उनके संगी उन लोगों की ऐसी लक्ष्योन्मुख प्रवृत्तियों का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि अन्ततः बुद्धिमान और प्रगतिशील ऐसे ही लोगों को माना जाता है, जो चित्त की चपलता को नियन्त्रित कर उसे अपने लक्ष्य की ओर ही लगाये रहते हैं—वह कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का, शरीर सौष्ठव का हो या आर्थिक समृद्धि का, कला-कौशल का हो या वैज्ञानिक आविष्कार का अथवा दार्शनिक चिन्तन-मनन का।
भारतीय मनीषियों ने मन को संस्कारित व परिष्कृत करने के लिए पंचकोशीय साधना विधान में मनोमय कोश की साधना का एक स्वतन्त्र चरण ही रखा है। मनोमय कोश का अर्थ है विचारशीलता विवेक बुद्धि।
मनोमय कोश अर्थ और साधना
मन कोई ऐसा तत्व नहीं है जो केवल मनुष्य के पास ही है। वह हर जीवित प्राणी के पास होता है। कीट पतंग भी उससे रहित नहीं हैं। परन्तु मनोमय कोश के व्याख्याकारों ने उसे दूरदर्शिता, तर्क प्रखरता एवं विवेक शीलता के रूप में विस्तार पूर्वक समझाया है। मन की स्थिति हवा की तरह है वह दिशा विशेष तक सीमित न रहकर स्वेच्छाचारी वन्य पशु की तरह किधर भी उछलता-कूदता है। पक्षियों की तरह किसी भी दिशा में चल पड़ता है। इसे दिशा देना, चिन्तन को अनुपयोगी प्रवाह में बहने से बचा कर उपयुक्त मार्ग पर सुनियोजित करना मनस्वी होने का प्रधान चिन्ह है। मनोनिग्रह-मनोजय इसी का नाम है। जंगली हाथी को पकड़ कर अनुशासित बनाने का काम तो कठिन है; पर इसकी उपयोगिता अत्यधिक है। जंगली हाथी फसलें उजाड़ते और झोंपड़ियां तोड़ते हैं और भूखे प्यासे अनिश्चित स्थिति में भटकते हैं। किन्तु पालतू बन जाने पर उनकी जीवन चर्या भी सुनिश्चित हो जाती है और साथ ही वे अपने मालिक का भी बहुत हित साधन करते हैं। सधे हुए मन की तुलना पालतू हाथी से की जा सकती है और अनियंत्रित मन की उन्मत्त जंगली हाथी कहा जा सकता है।
आवेग और आवेश ग्रस्त होकर उन उत्तेजनाओं से प्रेरित मनुष्य कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी कर गुजर सकता है। यह चिन्तन और कर्तृत्व इतना असंगत हो सकता है कि फलस्वरूप जीवन भर पश्चाताप करना पड़े और असीम हानि उठानी पड़े। किन्तु आवेगों के प्रवाह में बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और कुछ सूझ नहीं पड़ता। उन्मत्तों की तरह दूसरों की हत्या, आत्म हत्या न सही ऐसे काम तो सहज ही बन पड़ते हैं जिन पर शान्त मनःस्थिति में विचार करने पर स्वयं ही अपने पर क्रोश आता है। असंख्य मनुष्य ऐसे ही उद्धत कर्म करते हैं अथवा मरे हुए मन से अकर्मण्य बने हुए जीवन की लाश ढोते हैं। स्थिति से उबरने का कोई प्रकाश भी उन्हें नहीं मिलता। प्रायः एक समय में एक प्रकार के विचार एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यह प्रवाह जिधर भी चलता है उधर लाभ ही लाभ, औचित्य ही औचित्य दिखाई पड़ता है। जब कि वास्तविकता कुछ और ही होती है। प्रवाह को रोक कर, धारा द्वारा उससे बांध या बिजली घर बनाये जाते हैं। मन के प्रवाह को जिस दूसरी प्रतिरोध शक्ति से रोका जाता है, उचित अनुचित के मंथन से उलट-पुलट कर नवनीत निकाला जाता है, तब पता चलता है कि क्या सोचना सार्थक है क्या निरर्थक? लाभ किसमें है और हानि किसमें? उतत्काल के क्षणिक लाभ को ही सब कुछ न मान कर भविष्य के चिरस्थायी परिणाम का विचार करने में समर्थ एवं परिपक्व बुद्धि मन के प्रवाह को अवांछनीय दिशा में रोक सकती, उसे उचित में नियोजित कर सकती है। इस परिष्कृत चिन्तन प्रक्रिया को मनोमय कोष की उपलब्धि कह सकते हैं।
महा मनीषी, तत्व दर्शी, शोध कर्ता एवं मनस्वी व्यक्ति ही महा मानवों की पंक्ति में बैठ सकने में समर्थ हुए हैं। उनने संसार का नेतृत्व किया है और अपने महान कर्तृत्वों से इतिहास को यशस्वी किया है। इन सभी की यह प्रमुख विशेषता रही है कि उन्होंने अपने मन पर अंकुश करना और उसे दिशा देना सीखा। सामान्य लोगों का मन हवा के साथ उड़ते फिरने वाले तिनके की तरह अपनी मानसिक चेतना को निरर्थक अथवा अनर्थ मूलक स्थिति में भटकने देता है जबकि मनस्वी व्यक्ति उसकी प्रत्येक लहर को सुनियोजित करता है। उचित और अनुचित की कसौटी का अंकुश रख कर मन को उसी दिशा में, उसी गति से चलने देता है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण हित साधन हो सके।
इच्छाओं को मोड़ने में, चिन्तन को सुनियोजित करने में सफलता प्रखर-तर्क बुद्धि से उत्पन्न होती है और आत्म-दमन कर सकने की साहसिकता से मनोनिग्रह बन पड़ता है। एकाग्रता का, चित्त-वृत्ति निरोध का बहुत माहात्म्य योगशास्त्रों में बताया गया है। इसका अर्थ चिन्तन प्रक्रिया को ठप्प कर देना, एक ही ध्यान में निमग्न रहना नहीं, वरन् यह है कि विचारों का प्रवाह नियत निर्धारित प्रयोजन से ही पूर्वक लगा रहे। यह कुशलता जिनकी करतलगत हो जाती है वे जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं उसमें प्रायः अभीष्ट सफलता ही प्राप्त करके रहते हैं। बिखराव की दशा में चिन्तन की गहराई में उतरने का अवसर नहीं मिलता अस्तु किसी विषय में प्रवीणता और पारंगतता भी हाथ नहीं लगतीं। संसार में विशेषज्ञों का स्वागत होता है, यहां हर क्षेत्र में ‘ए-वन’ की मांग है और यह उपलब्धि कुशाग्र बुद्धि पर नहीं सघन मनोयोग के साथ सम्बद्ध है। यह मनोयोग का वरदान प्राप्त करने के लिए जो प्रयास व्यायाम करने पड़ते हैं उन्हें ही मनोमय कोश की साधना कहते हैं।
मनोमय कोश की साधना मस्तिष्कीय क्षेत्र में घुसे मनोविकारों को—दुष्प्रवृत्तियों को—निरस्त करने के लिए लड़ा जाने वाला महाभारत हो, साथ ही इसमें धर्म राज्य की—राम राज्य की—स्थापना का लक्ष्य संकल्प भी जुड़ा हुआ हो।
इस सन्दर्भ में वैज्ञानिक-अनुशीलन प्रयत्न ध्यान देने योग्य हैं। बहुत समय पहले शारीरिक रोगों का कारण, वात पित्त, कफ, अपच, मलावरोध, ऋतु प्रभाव, विषाणुओं का आक्रमण आदि माना जाता है नवीनतम शोधें शरीर पर पूरी तरह मनःसत्ता का अधिकार मानती हैं और बताती हैं कि बाह्य कारणों से उत्पन्न हुए रोग तो शरीर की जीवनी शक्ति स्वयं ही अच्छे कर लेती है अथवा मामूली से उपचार से वे अच्छे हो सकते हैं। जटिल रोग तो आमतौर से मनोविकारों के ही परिणाम होते हैं। उनका निराकरण दवा दारू से नहीं मानसिक परिशोधन से ही सम्भव हो सकता है।
शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों का भी यही प्रधान कारण है। दुष्कर्म अथवा दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों से भी ग्रसित रहते हैं। उन्माद विस्फोट की स्थिति न आये तो भी असन्तुलन से ग्रस्त व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त स्थिति में पड़े रहते हैं। अकारण दुःख पाते और अकारण दुःख देते हैं। इनकी मनःस्थिति कितनी दयनीय होती है यह देखने भर से बड़ा कष्ट होता है। शारीरिक व्यथाओं से पीड़ितों की अपेक्षा मनोवेगों से ग्रस्त लोगों की संख्या ही नहीं पीड़ा भी अधिक है। इन व्यथाओं से छुटकारे का उपाय अस्पतालों में नहीं, मानसिक संशोधन की साधनाओं पर ही अवलम्बित है। वे उपाय, उपचार अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के आधार पर उसे मनोमय कोश से, साधना से अधिक सुविधापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है।
काय-विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए ज्ञान तन्तु सारे शरीर में फैले हैं। उन्हीं के माध्यम से इस जटिल यन्त्र का संचालन होता है। इन्द्रियों की क्रियाशक्ति, अनुभूतियां, सरसताएं मस्तिष्क में ही जाकर खुलती हैं। इन्द्रिय गोलक तो मात्र सूचनाएं संग्रह करने और उन्हें मस्तिष्कीय केन्द्रों तक पहुंचाने भर का काम करते हैं। कोई मानसिक कष्ट होने पर सारा शरीर शिथिल हो जाता है और क्रियाशक्ति में स्पष्टतः अस्त-व्यस्तता दीखने लगती है। भय, चिन्ता, शोक, निराशा जैसे प्रसंगों पर किसी भी मनुष्य का चेहरा उदास और सारा शरीर शिथिल देखा जा सकता है। क्रोध, अपमान, द्वेष, प्रतिशोध की स्थिति में किस प्रकार अंग-प्रत्यंगों में उत्तेजना दीख जाती है, इसे किसी आवेशग्रस्त पर छाये हुए भावोन्माद को देख कर सहज ही देखा, समझा जा सकता है। प्रसन्न और निश्चिन्त रहने वाले स्वस्थ रहते और दीर्घजीवी बनते हैं। इसके विपरीत क्षुब्ध रहने वाले अकारण दुर्बल होते जाते हैं और अकाल मृत्यु से असमय मरते हैं। यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि शरीर संस्थान पर आहार-विहार का, जलवायु का जितना प्रभाव पड़ता है उससे कहीं अधिक भाव-संस्थान का होता है।
शरीर में स्नायुमण्डल द्वारा तथा नलिका विहीन ग्रन्थियों द्वारा भावनाएं क्रियाशील होती हैं। हमारे सम्पूर्ण शरीर में स्नायुओं का जाल बिछा हुआ है। सामान्यतः स्नायु उज्ज्वलवर्णी होते हैं और तार की तरह ठोस होते हैं। हमारी सभी पेशियां स्नायुओं के ही आधार पर चलती हैं। प्रत्येक पेशी में पहुंचने वाला मुक्ष्य स्नायु सुतली की तरह मोटा होता है। फिर उसकी शाखा-प्रशाखाएं अधिकाधिक पतली होती चली जाती हैं। कई प्रशाखाएं तो बारीक सूत जैसी पतली होती हैं।
सम्पूर्ण स्नायुमण्डल के दो भाग हैं—(1) ऐच्छिक (2) अनैच्छिक। चलने-फिरने, झुकने-मुड़ने, वस्तुएं उठाने, रखने आदि की क्रियाओं में हम अपने हाथ-पैर आदि को इच्छानुसार हिलाते हैं। यह ऐच्छिक स्नायुओं के ही कारण है। अनैच्छिक स्नायुओं पर हमारा ऐसा अधिकार नहीं होता। वे शरीर की आन्तरिक क्रियाएं सम्पादित करते हैं। जैसे हृदय की धड़कनें, सांसों का आना-जाना आदि।
अनैच्छिक स्नायुमण्डल का केन्द्र मस्तिष्क का एक लघु अंश हाइपोथेलेमस होता है। यही ‘हाइपोथेलेमस’ नारी व पौरुष ग्रन्थियों को भी नियन्त्रित करता है साथ ही ‘मोनोएमीन आक्सीडंज’ नामक किण्वज (एन्जाइम) भी सम्पूर्ण शरीर में विकर्ण होते हुए भी केन्द्रीय स्नायुविक प्रणाली में विशेष रूप से जमा रहता है। ‘हाइपोथेलेमस’ द्वारा पिट्यूटरी ग्रन्थि भी उत्तेजित होती है और उससे विभिन्न हार्मोन्स निकलते हैं जो भावनाओं का परिणाम भी होते हैं और नई भावनाओं का कारण भी। किसी नई परिस्थिति के उपस्थित होने पर नलिकाविहीन ग्रन्थियों पर दबाव पड़ता है और वे विभिन्न हारमोनों को स्रवित करती हैं। इन हारमोनों की शरीर में प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया उसी के अनुरूप भावना समूहों को जन्म देती है। जैसे किसी रोग के कीटाणुओं के संक्रमण-दबाव से पिट्यूटरी ग्रन्थि ने कोई हारमोन छोड़ा, इससे शरीर में तेज हलचल मच गई, व्यक्ति को अस्वस्थता महसूस होने लगी और वह खाट पर पड़ गया। अब बीमारी की दशा में तरह-तरह की भावनाएं जो अचेतन में दबी थीं, उभरने लगीं। उनके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी पैदा होने लगती हैं।
मनोमय कोश का निवास मस्तिष्क में बताये जाने का अर्थ केवल इतना ही है कि उसका केन्द्रीय कार्यालय वही है। उसके सूक्ष्म अवयव उसकी शाखा-प्रशाखायें तो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त-विस्तृत हैं। मस्तिष्क के जीवाणु अन्य जीवाणुओं से अधिक समझदार और अधिक अनुभवी होते हैं, इसीलिए वे शेष जीवाणुओं के अगुआ नेता कहे जाते हैं। वे जिस दिशा में चलते हैं, शेष जीवाणु भी उसी दिशा धारा में बहने लगते हैं। सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ,, प्रसन्न, उल्लसित, प्रगतिशील बनाये रखने के लिए मस्तिष्कीय-स्थिति वैसी होनी जरूरी है। नेता ही निराश-हताश, कुण्ठित-त्रस्त हुआ, तो प्रगति की क्या आशा की जा सकती है। नेता का संवेग समस्त अनुयायियों को प्रभावित करता है।
वियना के मनोचिकित्सक डा. फैंकल का मत है कि मानसिक-धरातल ही शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। मानसिक असन्तुलन का कारण जीवन की सार्थकता को न समझना है। इसीलिए उन्होंने ‘लौगोथेरेपी’ या ‘अर्थबोधचिकित्सा’ नाम की चिकित्सा पद्धति विकसित की है। डा. फैंकल की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन और कार्य की सार्थकता का बोध नहीं हो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन के लक्ष्य और उनकी सिद्धि ही आनन्द का आधार है। डा. फैंकल की चिकित्सा पद्धति में रोगी से प्रिय-अप्रिय सभी विषयों पर चर्चा कर, उसे जीवन की सार्थकता की तलाश की प्रेरणा दी जाती है। व्यक्ति को जैसे ही जीवन में सार्थकता की अनुभूति हो उठती है, वह अपने भीतर निहित शक्तियों का स्मरण कर आत्मविश्वास से भर उठता है और धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगता है। मनःक्षेत्र की स्वस्थता उसके स्थूल शरीर को भी स्वस्थ बना देती है। सूक्ष्म शरीर की हलचलों का स्थूल शरीर पर स्पष्ट एवं निश्चित परिणाम होता है। तन्त्रकीय रोगों का कारण दबे हुए गन्दे विचार ही होते हैं। शरीर-शास्त्रियों का भी मता है कि मात्र मानसिक-चित्रों के आधार पर ही अनेक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ‘‘इन्फ्लुएन्स आफ द माइन्ड अपान द बॉडी’’ नामक पुस्तक के लेखक डा. टुके ने लिखा है—‘‘विक्षिप्तता, मूढ़ता, अंगों का निकम्मा हो जाना, पित्त, पाण्डुरोग, केश-पतन, रक्ताल्पता, घबराहट, मूत्राशय के रोग, गर्भाशय में पड़े बच्चे का अंगभंग हो जाना, चर्म रोग, फुन्सियां, फोड़े, एग्जिमा आदि अनेक स्वास्थ्यनाशक रोग मात्र मानसिक क्षोभ तथा भावनात्मक उद्देलन के परिणाम होते हैं।’’ मानसिक क्षोभ, भावनात्मक उद्देलन, निषेधात्मक चिन्तन, सूक्ष्म शरीर की विकृतियां हैं, जिनका स्थूल शरीर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार परिष्कृत दृष्टिकोण स्वस्थ-उदात्त चिन्तन, आदर्शवादी विचारधारा सूक्ष्म-शरीर को तेजस्वी प्रखर बनाती है और उसकी श्रेष्ठ प्रभाव स्थूल शरीर पर भी स्पष्ट देखा जा सकता है।
विधेयात्मक विचारों की, ऊर्ध्वमुखी चिन्तन की आश्चर्यजनक महत्ता के प्रतिपादन में डा. बैनेट ने स्वयं को ही प्रस्तुत किया है। 50 वर्ष की आयु तक डा. बैनेट निराशा और अवांछनीय चिन्तन के कारण अपना स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा बैठे। उन्हें जब ऊर्ध्वगामी चिन्तन की इस असीम उपादेयता का पता चला तो उन्होंने अपना जीवन क्रम ही बदल डाला। मन की जड़ता और विषय-विचारों का जुआ उनने उतार फेंका, हृदय को श्रद्धा आस्था से भरा, सदैव प्रसन्न प्रफुल्ल रहने की आदत बनाली। 20 वर्षों के अपने इस जीवन को स्वर्गीय सुख से ओत-प्रोत बनाते हुए डॉ. बैनेट ने अपनी 50 वर्षीय फोटो तथा 70 वर्षीय फोटो भी एक पुस्तक में छापी है। पहली में उनका चेहरा झुर्रियों से पिचके गाल, धंसी आंखों के कारण मनहूस दिखाई देता है जबकि 70 वर्ष की आयु में वे स्वस्थ सशक्त दिखाई देते हैं, झुर्रियां न जाने कहां चली गईं, चेहरे में उद्दीप्ति है और युवकों जैसी सक्रियता।
अब तक किये गये ऐसे ही विविध आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि मन का, मस्तिष्क का कष्ट प्रत्येक जीवाणु को कष्ट में डाल देता है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध का अनिष्ट प्रभाव समस्त जीवाणुओं में तुरन्त दौड़ जाता है, झलक उठता है। मस्तिष्क में प्रसन्नता का भाव आते ही प्रत्येक जीवाणु प्रसन्न-पुलकित हो उठता है। ये सभी जीवाणु परस्पर गहन आत्मीयता और अभिन्नता का भाव रखते हैं। प्रत्येक जीवाणु की दशा से सभी प्रभावित होते हैं—इनका सुख-दुःख मिला-जुला ही होता है। इनका पारस्परिक सौहार्द्र-सद्भावना अनूठा है। सच्ची मैत्री, प्रगाढ़ आत्मीयता समानुभूति के ये अनूठे उदाहरण हैं। कल्पना करें कि एक व्यक्ति को तेज भूख लगी है। सुस्वादु भोजन का थाल सामने है। उसी समय किसी प्रियजन की मृत्यु का तार मिलता है। उसे पढ़ते ही मस्तिष्क में उस प्रियजन की संचित स्मृति सहसा जागृत हो उठती है। मन में आत्मीय सम्वेदना उमड़ पड़ती है। मस्तिष्क के जीवाणुओं में हलचल, उथल-पुथल मच जाती है। मस्तिष्क के जीवाणुओं की इस प्रतिक्रिया का तत्काल सम्पूर्ण शरीर के जीवाणुओं पर प्रभाव पड़ता है। जीभ सूखने लगती है। भूख बढ़ाने वाले जीवाणु जो उछल-कूद मचा रहे थे, चीख-चीखकर भोजन की मांग कर रहे थे, सहमकर शान्त, निष्क्रिय, दुबके-से बैठ जाते हैं। हृदय और दूसरे अंग भी निष्प्राण से हो चलते हैं। दिल-डूबने लगता है, आंखों के सामने अन्धेरा छा जाता है, शरीर निढाल हो जाता है। समस्त अंगों पर यह प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि मस्तिष्कीय जीवाणुओं की भावदशा का तत्काल प्रभाव सम्पूर्ण शरीरस्थ जीवाणु-समूहों पर पड़ता है।
‘ओल्ड एज : इट्स काफ एन्ड प्रिवेन्शन’ नामक पुस्तक में उसके रचियता सुप्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक तथा लेखक डा. बैनेट ने एक बहुत ही मनोरंजक किन्तु शिक्षाप्रद घटना दी है। एक 19 वर्षीय फ्रान्सीसी युवती ने एक अमेरिकन नव-युवक से विवाह का निश्चय किया। युवक निर्धन था सो यह तय हुआ कि पहले वह अमेरिका जाकर धन कमायेगा और लौटकर शादी करेगा। युवक ने 3 वर्ष में पर्याप्त धन कमा लिया, पर दुर्भाग्य से कोई मुकदमा लग जाने के कारण वह 15 वर्ष तक फ्रान्स नहीं लौट सका। 15 वर्ष बाद जब वह वापस लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी मंगेतर का स्वास्थ्य, सौन्दर्य बिलकुल वैसा ही है जैसा वह 19 वर्ष पूर्व था। 34 वर्ष की अधेड़ अवस्था हो जाने पर उसमें 19 वर्षीय नव-युवती के गुण विद्यमान थे।
घटना का विवेचन करते हुये बैनेट महोदय लिखते हैं—प्रकृति ने मनुष्य शरीर की संचालन क्रिया प्रक्रिया इस प्रकार रखी है कि शरीर का प्रत्येक कोश (सैल) 80 दिन पीछे पुराना होकर मैल के रूप में उसी प्रकार बाहर निकल जाता है, जिस प्रकार समुद्री लहरों में निरन्तर ज्वार भाटे से समुद्र की गन्दगी तटों पर जमा होती रहती है। कोश-परिवर्तन की यह प्रक्रिया आयु बढ़ने के साथ क्षीण होती रहती है, उसी का नाम वृद्धावस्था है—किन्तु इस घटना ने इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही उलट दिया, ऐसा क्यों?
इसका उत्तर युवती के मुंह से दिलवाते हुये श्री बैनेट लिखते हैं कि—मैं प्रतिदिन प्रातःकाल एक आदमकद शीशे के सम्मुख खड़ी होकर अपना चेहरा देखती और मन की मन अनुभव करती की मैं ठीक वैसी ही हूं जैसी कल थी। दिन के परिवर्तन ने मेरे शरीर में कोई प्रभाव नहीं डाला इच्छा शक्ति की यह दृढ़ता मुझे दिन भर पुलकित और प्रसन्न बनाये रखती। उसी का फल है जो मैं जैसी 15 वर्ष पूर्व थी वैसी ही आज भी हूं।’’ सूक्ष्म शरीर के शोधन की विचारों को ऊंचा उठाने की संकल्प की महत्ता उन्होंने अमरीका के अध्यात्म परायण व्यक्ति डॉ. मारडन की पुस्तक ‘‘लौह इच्छा शक्ति’’ (ऐन आइरन विल) से समझी। जिसमें बताया गया है—‘‘मनुष्य अपने विचार नये करले, चरित्र को ऊंचा उठाले तो अपना शरीर ही बदल सकता है।’’ यह स्वाध्याय उनके लिये तो औषधि बना ही, सैकड़ों को नया जीवन देने वाला है। प्रेम, मैत्री, दया, करुणा और परोपकारी विचारों को धारण कर कोई भी इसका प्रत्यक्ष लाभ ले सकता है।
खोपड़ी के ऊपर या नीचे की रक्तवाहनियों की पेशियां भावनाओं के अनुसार फैलती-सिकुड़ती व तीव्र सम्वेदनात्मक प्रतिक्रियायें करती हैं।
अस्वस्थ भावनाएं विभिन्न शारीरिक रोगों का कारण बनती हैं। सामान्य सिर दर्द से लेकर ‘‘माइग्रेन’’ नामक कठिन सिर दर्द भावनात्मक तनाव से होता है। इस तनाव से खोपड़ी की रक्तवाहनियां सिकुड़ती हैं और इससे सिर दर्द शुरू हो जाता है। आज तो यह पाया जाता है कि सिर दर्द की सी घटनाओं में से पचासी का कारण भावनात्मक तनाव होता है।
भावना-क्षोभ के कारण पेशियों में उत्पन्न तनाव के कारण कई बार लोग भोजन के बाद ऐसा अनुभव करते हैं कि कलेजे पर बोझ आ पड़ा है और भोजन नीचे सरक ही नहीं रहा है। अधिक तनाव होने पर उबकाई आने लगती है, जी मिचलाने लगता है।
भावनात्मक तनाव से उत्पन्न स्नायु-रोगों में डकारें आना, पेट में ऐंठन होना, विभिन्न वायु-विकार अनेक त्वचा-विकार, एग्जिमा, खुजली आदि होते हैं।
कमर-दर्द के बारे में अब ऐसा ज्ञात हुआ है कि अधिकांश मामलों में इसका कारण भावनात्मक तनाव ही होता है। यह जान लेने पर कि भावनात्मक तनावों एवं विकृतियों से ही अधिकांश रोग पैदा होते हैं, यह प्रश्न अनेकों को कचोटता है कि भावनाओं पर नियन्त्रण कैसे हो? इसका एक ही सरल मार्ग है—समझदारी भरे दृष्टिकोण का नित्य-प्रति के जीवन में अभ्यास। बिना अभ्यास के यह दृष्टिकोण व्यावहारिक जीवन में नहीं उतरता। जिन्दगी को बोझ न मानते हुए खेल-भावना से जीना, अभ्यास द्वारा ही सम्भव है। अपनी सीमाओं को पहचानना, शक्ति के सर्वोत्तम उपयोग की व्यवस्था करना, ‘मैं-मैं’ की चीख-पुकार से मुक्त होकर अपने दायित्वों को समझना और निभाना, तथा सृजनात्मक वृत्तियों का जीवन में निरन्तर विकास करना ही एक मेध राजमार्ग है।
सामान्यतः कठोरता, क्रोध, बात-बात में लड़ बैठने आदि को हम भ्रान्तिवश शक्ति का पर्याय मान बैठते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक इस सबको ‘बचकानी हरकतें’ मानते हैं। ये दुर्बलता के प्रतीक हैं। शक्तिशाली व्यक्ति विनम्र एवं दृढ़ होता है। क्रोध और झगड़ालूपन तो शक्तिहीनता की उपज है। सादगी-संयम का अभ्यास ही शक्ति का स्रोत है। किन्तु अपनी दुर्बलताओं पर व्यर्थ की खीझ भी लाभकर न होगी। धीरे-धीरे ही कुसंस्कार चित तल पर जमते हैं और धीरे-धीरे ही उनका उन्मूलन सम्भव है। सतत् अभ्यास ही सर्वोत्तम उपचार है। इस बात को सदा ध्यान में रखा जाय कि मन की कुटिलता ओर अनैतिक कर्म ही रोग का आधार हैं तथा मन की शुचिता, स्नेह, करुणा और व्यापक मानवीय प्रेम द्वारा इन रोगों को मिटा सकना सरलता से सम्भव है।
मस्तिष्क की धुलाई-सफाई वैज्ञानिक उपकरणों से भी सम्भव हो सकती है। फिर अध्यात्म साधना के उपचार तो उससे अधिक ही सशक्त समर्थ होते हैं। उनका प्रभाव तो और भी अधिक होना चाहिये।
लेऐलेक्ट्रिकल स्टीम्यूलेशन आफ ब्रेन (ई.एस.बी.) पद्धति के अनुसार कई एशियन विश्वविद्यालयों ने आंशिक रूप से मस्तिष्क की धुलाई (ब्रेन वाशिंग) में सफलता प्राप्त करली है। अभी यह बन्दर, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे जैसे छोटे स्तर के जीवों पर ही प्रयोग किये गये हैं। आहार की रुचि, शत्रुता, मित्रता, भय, आक्रमण आदि आदि के सामान्य स्वभाव को जिस प्रकार चरितार्थ किया जाना चाहिए उसे वे बिलकुल भूल जाते हैं और विचित्र प्रकार का आचरण करते हैं। बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा गया तो वह आक्रमण करना तो दूर उससे डर कर एक कोने में जा छिपी। क्षणभर में एक-दूसरे पर खूनी आक्रमण करना, एक आध मिनट बाद परस्पर लिपट कर प्यार करना यह परिवर्तन उस विद्युत क्रिया से होता है जो उनके मस्तिष्कीय कोषों के साथ सम्बद्ध रहती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू हो सकती है। मानव मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत होता है उसमें प्रतिरोधक शक्ति भी अधिक होती है इसलिए उसमें हेर-फेर करने के लिए प्रयास भी कुछ अधिक करने पड़ेंगे और सफलता प्राप्त करने में देरी भी लगेगी, पर जो सिद्धांत स्पष्ट हो गये हैं उनके आधार पर यह निश्चित हो गया है कि मनुष्य को भी जैसा चाहे सोचने, मान्यता बनाने और गतिविधियां अपनाने के लिए विवश किया जा सकता है।
मनोमय कोश की साधना मस्तिष्कीय क्षेत्र की धुलाई सफाई ही नहीं करता, वरन् उसे समुन्नत सुसज्जित एवं सुसंस्कृत बनाने का काम भी बहुत हद तक पूरा कर सकती है। मनोमय कोश शरीर और मस्तिष्क के समूचे क्षेत्र को अपने अंचल में समेटे हुए हैं। वह इन दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अन्तःकरण के अस्त-व्यस्त और विकृत स्थिति से बने रहने पर उसकी प्रतिक्रिया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। व्यक्तित्व लड़खड़ा जाने पर दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों ही गड़बड़ाते हैं। फलतः गतिविधियां अवांछनीयता से भर जाती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में विपत्तियां ही उत्पन्न होंगी। अवरोध ही खड़े होंगे। कलह और संकट आक्रमण करेंगे। समूचा जीवन ही नरक बन जायगा। इस नारकीय यन्त्रणा से छुटकारा कोई और नहीं दिला सकता। क्योंकि इस विपत्ति का दोष भले ही किसी पर थोपा जा सके उसका कारण अपना आपा ही होता है। मनःस्थिति के अनुरूप परिस्थिति बनने का तथ्य इतना स्पष्ट है कि उसे झुठलाये जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अपने आप में परिवर्तन किये बिना हम इस नरक से अन्य किसी तरह उबर नहीं सकते। जीवनक्रम में उत्पन्न विविध-विधि अवरोधों से छुटकारा पाये बिना हमारा उद्धार हो नहीं सकता। समस्याओं और विपन्नताओं से त्राण मिल नहीं सकता।
समृद्धि, प्रगति और सुख-शान्ति की समस्त सम्भावनायें बीज रूप में अपने ही भीतर भरी पड़ी हैं। सत्प्रवृत्तियों की देवी और सद्भावनाओं के देवता ही हमें दिव्य वरदानों से सुसम्पन्न बनाते हैं। अन्तरंग की विभूतियां ही बहिरंग की सिद्धियां बन कर सामने आती हैं। आत्मशोधन और आत्म परिष्कार जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। इसे प्रत्यक्ष कल्प-वृक्ष की उपमा दी जा सकती है।
मनोमय कोश का विज्ञान और साधन हमारी मानसिक स्थिति के परिष्कार का ऋषि प्रणीत उपाय है। इस दिशा में कदम बढ़ाने पर हम हर दृष्टि से लाभान्वित ही होते हैं।
यही सधा हुआ मन आत्मिक क्षेत्र में लगाये जाने पर सुषुप्त शक्ति केन्द्रों को जागृत व क्रियाशील बनाता है और दिव्य क्षमताएं प्रकाश में आती हैं। अन्तश्चेतना का परिष्कार सामान्य व्यक्ति को महामानव स्तर पर ले जाकर ही रहता है। प्रगति का सम्पूर्ण इतिहास मनःशक्ति के पुंजीभूत, लक्ष्य केन्द्रित पुरुषार्थ की ही यश गाथा है। चंचलता का प्रकृति को पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में परिवर्तित करने का पराक्रम ही प्रगति का सार्वभौम आधार रहा है।
मन की दूसरी प्रवृत्ति है—सुख लिप्सा। शारीरिक सुखों के भोग का माध्यम है—इन्द्रियां। उनके द्वारा विभिन्न वासनाओं का स्वाद मिलता है। पेट और प्रजनन से सम्बन्धित सुखों के लिए तरह-तरह की चेष्टाओं में ही मल उलझा रहता है और इन सुखों की प्रापित के लिए प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि इनकी मात्र कल्पनाएं करने में भी बहुत अधिक समय नष्ट करता है। फिर इन भौतिक सुखों के लिए साधन जुटाने में भी मन को जाने कितने ताने-बाने बुनने पड़ते हैं। इन्द्रियों की प्रिय वस्तु या व्यक्ति देखने, सुनने, छूने, सूंघने अथवा स्वाद लेने की लिप्साएं मन को ललक से भर देती हैं और वह उसी दिशा में लगा रहता है। अहंकार की पूर्ति के लिए मन औरों पर प्रभाव डालने हेतु तरह तरह की चेष्टाएं करता है और व्यक्ति भांति-भांति ठाट-बाट बनाता है। संग्रह और स्वामित्व की इच्छाएं भी अनेक विधि प्रयत्नों का कारण बनती हैं। इन सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं की प्यास को व्यक्त करने के लिए ही तृष्णा शब्द का प्रयोग होता है। अहं-भावना पर आघात पहुंचते ही प्रतिशोध की उत्तेजना प्रबल हो उठती है। इच्छित विषय पर अपना हक मान लेना और फिर उसके न प्राप्त होने या प्राप्ति में बाधा पड़ने पर भड़क उठना भी, अहंता पर आघात के ही कारण होता है। यह उत्तेजना ही क्रोध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि सम्पूर्ण विकार-समूह वस्तुतः मन में उठने वाली प्रतिक्रियाएं मात्र हैं, जो भौतिक सुख की लिप्साओं के कारण उठती रहती हैं। लिप्सा की इस ललक की दिशा को उलट देना ही तप है। वह दूसरी दिशा भौतिक सुखों की वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति से होने वाले क्षणिक सुखों को नहीं है। वरन् आनन्द की है। आनन्द उपभोग से नहीं, उत्कर्ष और उत्सर्ग से प्राप्त होता है। सुख मन का विषय है, जब कि आनन्द और आत्म-सन्तोष आत्मा का। सुख लिप्सा का अभ्यस्त मन आनन्द के अस्वाद को नहीं जान पाता और जिसे जाना ही नहीं, उसके प्रति गहरी स्थायी प्रीति, सच्चा आकर्षण सम्भव नहीं। आनन्द की आकांक्षा विषय-लोलुप मन में प्रगाढ़ नहीं होती। उसके लिए तो मन का प्रशिक्षण आवश्यक है। यह प्रशिक्षण—प्रक्रिया ही तप है। तपस्वी को कष्ट इसी अर्थ में सहना पड़ता है, कि अभ्यस्त सुख का अवसर जाता रहता है। शारीरिक सुख-सुविधाएं सिमटती हैं, मानसिक आमोद-प्रमोद का भी अवकाश नहीं रहता और आदर्श-निष्ठ आचरण आर्थिक समृद्धि के भी आड़े ही आता है। प्रत्यक्ष तौर पर तो, ऐसे परिणामों के लिए किया जाने वाला प्रयास मूर्खता ही प्रतीत होगा।
लेकिन श्रेष्ठ उपलब्धियों का राज-मार्ग यही है किसान, विद्यार्थी, पहलवान, श्रमिक, व्यवसायी, कलाकार आदि को भी अपनी प्रगति की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए बाल-चंचलता से मन को विरत ही करना पड़ता है और अपने नीरस प्रयोजनों में ही मनःशक्ति नियोजित करनी पड़ती है। शौक-मौज के अभ्यस्त उनके संगी उन लोगों की ऐसी लक्ष्योन्मुख प्रवृत्तियों का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि अन्ततः बुद्धिमान और प्रगतिशील ऐसे ही लोगों को माना जाता है, जो चित्त की चपलता को नियन्त्रित कर उसे अपने लक्ष्य की ओर ही लगाये रहते हैं—वह कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का, शरीर सौष्ठव का हो या आर्थिक समृद्धि का, कला-कौशल का हो या वैज्ञानिक आविष्कार का अथवा दार्शनिक चिन्तन-मनन का।
भारतीय मनीषियों ने मन को संस्कारित व परिष्कृत करने के लिए पंचकोशीय साधना विधान में मनोमय कोश की साधना का एक स्वतन्त्र चरण ही रखा है। मनोमय कोश का अर्थ है विचारशीलता विवेक बुद्धि।
मनोमय कोश अर्थ और साधना
मन कोई ऐसा तत्व नहीं है जो केवल मनुष्य के पास ही है। वह हर जीवित प्राणी के पास होता है। कीट पतंग भी उससे रहित नहीं हैं। परन्तु मनोमय कोश के व्याख्याकारों ने उसे दूरदर्शिता, तर्क प्रखरता एवं विवेक शीलता के रूप में विस्तार पूर्वक समझाया है। मन की स्थिति हवा की तरह है वह दिशा विशेष तक सीमित न रहकर स्वेच्छाचारी वन्य पशु की तरह किधर भी उछलता-कूदता है। पक्षियों की तरह किसी भी दिशा में चल पड़ता है। इसे दिशा देना, चिन्तन को अनुपयोगी प्रवाह में बहने से बचा कर उपयुक्त मार्ग पर सुनियोजित करना मनस्वी होने का प्रधान चिन्ह है। मनोनिग्रह-मनोजय इसी का नाम है। जंगली हाथी को पकड़ कर अनुशासित बनाने का काम तो कठिन है; पर इसकी उपयोगिता अत्यधिक है। जंगली हाथी फसलें उजाड़ते और झोंपड़ियां तोड़ते हैं और भूखे प्यासे अनिश्चित स्थिति में भटकते हैं। किन्तु पालतू बन जाने पर उनकी जीवन चर्या भी सुनिश्चित हो जाती है और साथ ही वे अपने मालिक का भी बहुत हित साधन करते हैं। सधे हुए मन की तुलना पालतू हाथी से की जा सकती है और अनियंत्रित मन की उन्मत्त जंगली हाथी कहा जा सकता है।
आवेग और आवेश ग्रस्त होकर उन उत्तेजनाओं से प्रेरित मनुष्य कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी कर गुजर सकता है। यह चिन्तन और कर्तृत्व इतना असंगत हो सकता है कि फलस्वरूप जीवन भर पश्चाताप करना पड़े और असीम हानि उठानी पड़े। किन्तु आवेगों के प्रवाह में बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और कुछ सूझ नहीं पड़ता। उन्मत्तों की तरह दूसरों की हत्या, आत्म हत्या न सही ऐसे काम तो सहज ही बन पड़ते हैं जिन पर शान्त मनःस्थिति में विचार करने पर स्वयं ही अपने पर क्रोश आता है। असंख्य मनुष्य ऐसे ही उद्धत कर्म करते हैं अथवा मरे हुए मन से अकर्मण्य बने हुए जीवन की लाश ढोते हैं। स्थिति से उबरने का कोई प्रकाश भी उन्हें नहीं मिलता। प्रायः एक समय में एक प्रकार के विचार एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यह प्रवाह जिधर भी चलता है उधर लाभ ही लाभ, औचित्य ही औचित्य दिखाई पड़ता है। जब कि वास्तविकता कुछ और ही होती है। प्रवाह को रोक कर, धारा द्वारा उससे बांध या बिजली घर बनाये जाते हैं। मन के प्रवाह को जिस दूसरी प्रतिरोध शक्ति से रोका जाता है, उचित अनुचित के मंथन से उलट-पुलट कर नवनीत निकाला जाता है, तब पता चलता है कि क्या सोचना सार्थक है क्या निरर्थक? लाभ किसमें है और हानि किसमें? उतत्काल के क्षणिक लाभ को ही सब कुछ न मान कर भविष्य के चिरस्थायी परिणाम का विचार करने में समर्थ एवं परिपक्व बुद्धि मन के प्रवाह को अवांछनीय दिशा में रोक सकती, उसे उचित में नियोजित कर सकती है। इस परिष्कृत चिन्तन प्रक्रिया को मनोमय कोष की उपलब्धि कह सकते हैं।
महा मनीषी, तत्व दर्शी, शोध कर्ता एवं मनस्वी व्यक्ति ही महा मानवों की पंक्ति में बैठ सकने में समर्थ हुए हैं। उनने संसार का नेतृत्व किया है और अपने महान कर्तृत्वों से इतिहास को यशस्वी किया है। इन सभी की यह प्रमुख विशेषता रही है कि उन्होंने अपने मन पर अंकुश करना और उसे दिशा देना सीखा। सामान्य लोगों का मन हवा के साथ उड़ते फिरने वाले तिनके की तरह अपनी मानसिक चेतना को निरर्थक अथवा अनर्थ मूलक स्थिति में भटकने देता है जबकि मनस्वी व्यक्ति उसकी प्रत्येक लहर को सुनियोजित करता है। उचित और अनुचित की कसौटी का अंकुश रख कर मन को उसी दिशा में, उसी गति से चलने देता है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण हित साधन हो सके।
इच्छाओं को मोड़ने में, चिन्तन को सुनियोजित करने में सफलता प्रखर-तर्क बुद्धि से उत्पन्न होती है और आत्म-दमन कर सकने की साहसिकता से मनोनिग्रह बन पड़ता है। एकाग्रता का, चित्त-वृत्ति निरोध का बहुत माहात्म्य योगशास्त्रों में बताया गया है। इसका अर्थ चिन्तन प्रक्रिया को ठप्प कर देना, एक ही ध्यान में निमग्न रहना नहीं, वरन् यह है कि विचारों का प्रवाह नियत निर्धारित प्रयोजन से ही पूर्वक लगा रहे। यह कुशलता जिनकी करतलगत हो जाती है वे जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं उसमें प्रायः अभीष्ट सफलता ही प्राप्त करके रहते हैं। बिखराव की दशा में चिन्तन की गहराई में उतरने का अवसर नहीं मिलता अस्तु किसी विषय में प्रवीणता और पारंगतता भी हाथ नहीं लगतीं। संसार में विशेषज्ञों का स्वागत होता है, यहां हर क्षेत्र में ‘ए-वन’ की मांग है और यह उपलब्धि कुशाग्र बुद्धि पर नहीं सघन मनोयोग के साथ सम्बद्ध है। यह मनोयोग का वरदान प्राप्त करने के लिए जो प्रयास व्यायाम करने पड़ते हैं उन्हें ही मनोमय कोश की साधना कहते हैं।
मनोमय कोश की साधना मस्तिष्कीय क्षेत्र में घुसे मनोविकारों को—दुष्प्रवृत्तियों को—निरस्त करने के लिए लड़ा जाने वाला महाभारत हो, साथ ही इसमें धर्म राज्य की—राम राज्य की—स्थापना का लक्ष्य संकल्प भी जुड़ा हुआ हो।
इस सन्दर्भ में वैज्ञानिक-अनुशीलन प्रयत्न ध्यान देने योग्य हैं। बहुत समय पहले शारीरिक रोगों का कारण, वात पित्त, कफ, अपच, मलावरोध, ऋतु प्रभाव, विषाणुओं का आक्रमण आदि माना जाता है नवीनतम शोधें शरीर पर पूरी तरह मनःसत्ता का अधिकार मानती हैं और बताती हैं कि बाह्य कारणों से उत्पन्न हुए रोग तो शरीर की जीवनी शक्ति स्वयं ही अच्छे कर लेती है अथवा मामूली से उपचार से वे अच्छे हो सकते हैं। जटिल रोग तो आमतौर से मनोविकारों के ही परिणाम होते हैं। उनका निराकरण दवा दारू से नहीं मानसिक परिशोधन से ही सम्भव हो सकता है।
शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों का भी यही प्रधान कारण है। दुष्कर्म अथवा दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों से भी ग्रसित रहते हैं। उन्माद विस्फोट की स्थिति न आये तो भी असन्तुलन से ग्रस्त व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त स्थिति में पड़े रहते हैं। अकारण दुःख पाते और अकारण दुःख देते हैं। इनकी मनःस्थिति कितनी दयनीय होती है यह देखने भर से बड़ा कष्ट होता है। शारीरिक व्यथाओं से पीड़ितों की अपेक्षा मनोवेगों से ग्रस्त लोगों की संख्या ही नहीं पीड़ा भी अधिक है। इन व्यथाओं से छुटकारे का उपाय अस्पतालों में नहीं, मानसिक संशोधन की साधनाओं पर ही अवलम्बित है। वे उपाय, उपचार अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के आधार पर उसे मनोमय कोश से, साधना से अधिक सुविधापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है।
काय-विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए ज्ञान तन्तु सारे शरीर में फैले हैं। उन्हीं के माध्यम से इस जटिल यन्त्र का संचालन होता है। इन्द्रियों की क्रियाशक्ति, अनुभूतियां, सरसताएं मस्तिष्क में ही जाकर खुलती हैं। इन्द्रिय गोलक तो मात्र सूचनाएं संग्रह करने और उन्हें मस्तिष्कीय केन्द्रों तक पहुंचाने भर का काम करते हैं। कोई मानसिक कष्ट होने पर सारा शरीर शिथिल हो जाता है और क्रियाशक्ति में स्पष्टतः अस्त-व्यस्तता दीखने लगती है। भय, चिन्ता, शोक, निराशा जैसे प्रसंगों पर किसी भी मनुष्य का चेहरा उदास और सारा शरीर शिथिल देखा जा सकता है। क्रोध, अपमान, द्वेष, प्रतिशोध की स्थिति में किस प्रकार अंग-प्रत्यंगों में उत्तेजना दीख जाती है, इसे किसी आवेशग्रस्त पर छाये हुए भावोन्माद को देख कर सहज ही देखा, समझा जा सकता है। प्रसन्न और निश्चिन्त रहने वाले स्वस्थ रहते और दीर्घजीवी बनते हैं। इसके विपरीत क्षुब्ध रहने वाले अकारण दुर्बल होते जाते हैं और अकाल मृत्यु से असमय मरते हैं। यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि शरीर संस्थान पर आहार-विहार का, जलवायु का जितना प्रभाव पड़ता है उससे कहीं अधिक भाव-संस्थान का होता है।
शरीर में स्नायुमण्डल द्वारा तथा नलिका विहीन ग्रन्थियों द्वारा भावनाएं क्रियाशील होती हैं। हमारे सम्पूर्ण शरीर में स्नायुओं का जाल बिछा हुआ है। सामान्यतः स्नायु उज्ज्वलवर्णी होते हैं और तार की तरह ठोस होते हैं। हमारी सभी पेशियां स्नायुओं के ही आधार पर चलती हैं। प्रत्येक पेशी में पहुंचने वाला मुक्ष्य स्नायु सुतली की तरह मोटा होता है। फिर उसकी शाखा-प्रशाखाएं अधिकाधिक पतली होती चली जाती हैं। कई प्रशाखाएं तो बारीक सूत जैसी पतली होती हैं।
सम्पूर्ण स्नायुमण्डल के दो भाग हैं—(1) ऐच्छिक (2) अनैच्छिक। चलने-फिरने, झुकने-मुड़ने, वस्तुएं उठाने, रखने आदि की क्रियाओं में हम अपने हाथ-पैर आदि को इच्छानुसार हिलाते हैं। यह ऐच्छिक स्नायुओं के ही कारण है। अनैच्छिक स्नायुओं पर हमारा ऐसा अधिकार नहीं होता। वे शरीर की आन्तरिक क्रियाएं सम्पादित करते हैं। जैसे हृदय की धड़कनें, सांसों का आना-जाना आदि।
अनैच्छिक स्नायुमण्डल का केन्द्र मस्तिष्क का एक लघु अंश हाइपोथेलेमस होता है। यही ‘हाइपोथेलेमस’ नारी व पौरुष ग्रन्थियों को भी नियन्त्रित करता है साथ ही ‘मोनोएमीन आक्सीडंज’ नामक किण्वज (एन्जाइम) भी सम्पूर्ण शरीर में विकर्ण होते हुए भी केन्द्रीय स्नायुविक प्रणाली में विशेष रूप से जमा रहता है। ‘हाइपोथेलेमस’ द्वारा पिट्यूटरी ग्रन्थि भी उत्तेजित होती है और उससे विभिन्न हार्मोन्स निकलते हैं जो भावनाओं का परिणाम भी होते हैं और नई भावनाओं का कारण भी। किसी नई परिस्थिति के उपस्थित होने पर नलिकाविहीन ग्रन्थियों पर दबाव पड़ता है और वे विभिन्न हारमोनों को स्रवित करती हैं। इन हारमोनों की शरीर में प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया उसी के अनुरूप भावना समूहों को जन्म देती है। जैसे किसी रोग के कीटाणुओं के संक्रमण-दबाव से पिट्यूटरी ग्रन्थि ने कोई हारमोन छोड़ा, इससे शरीर में तेज हलचल मच गई, व्यक्ति को अस्वस्थता महसूस होने लगी और वह खाट पर पड़ गया। अब बीमारी की दशा में तरह-तरह की भावनाएं जो अचेतन में दबी थीं, उभरने लगीं। उनके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी पैदा होने लगती हैं।
मनोमय कोश का निवास मस्तिष्क में बताये जाने का अर्थ केवल इतना ही है कि उसका केन्द्रीय कार्यालय वही है। उसके सूक्ष्म अवयव उसकी शाखा-प्रशाखायें तो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त-विस्तृत हैं। मस्तिष्क के जीवाणु अन्य जीवाणुओं से अधिक समझदार और अधिक अनुभवी होते हैं, इसीलिए वे शेष जीवाणुओं के अगुआ नेता कहे जाते हैं। वे जिस दिशा में चलते हैं, शेष जीवाणु भी उसी दिशा धारा में बहने लगते हैं। सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ,, प्रसन्न, उल्लसित, प्रगतिशील बनाये रखने के लिए मस्तिष्कीय-स्थिति वैसी होनी जरूरी है। नेता ही निराश-हताश, कुण्ठित-त्रस्त हुआ, तो प्रगति की क्या आशा की जा सकती है। नेता का संवेग समस्त अनुयायियों को प्रभावित करता है।
वियना के मनोचिकित्सक डा. फैंकल का मत है कि मानसिक-धरातल ही शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। मानसिक असन्तुलन का कारण जीवन की सार्थकता को न समझना है। इसीलिए उन्होंने ‘लौगोथेरेपी’ या ‘अर्थबोधचिकित्सा’ नाम की चिकित्सा पद्धति विकसित की है। डा. फैंकल की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन और कार्य की सार्थकता का बोध नहीं हो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन के लक्ष्य और उनकी सिद्धि ही आनन्द का आधार है। डा. फैंकल की चिकित्सा पद्धति में रोगी से प्रिय-अप्रिय सभी विषयों पर चर्चा कर, उसे जीवन की सार्थकता की तलाश की प्रेरणा दी जाती है। व्यक्ति को जैसे ही जीवन में सार्थकता की अनुभूति हो उठती है, वह अपने भीतर निहित शक्तियों का स्मरण कर आत्मविश्वास से भर उठता है और धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगता है। मनःक्षेत्र की स्वस्थता उसके स्थूल शरीर को भी स्वस्थ बना देती है। सूक्ष्म शरीर की हलचलों का स्थूल शरीर पर स्पष्ट एवं निश्चित परिणाम होता है। तन्त्रकीय रोगों का कारण दबे हुए गन्दे विचार ही होते हैं। शरीर-शास्त्रियों का भी मता है कि मात्र मानसिक-चित्रों के आधार पर ही अनेक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ‘‘इन्फ्लुएन्स आफ द माइन्ड अपान द बॉडी’’ नामक पुस्तक के लेखक डा. टुके ने लिखा है—‘‘विक्षिप्तता, मूढ़ता, अंगों का निकम्मा हो जाना, पित्त, पाण्डुरोग, केश-पतन, रक्ताल्पता, घबराहट, मूत्राशय के रोग, गर्भाशय में पड़े बच्चे का अंगभंग हो जाना, चर्म रोग, फुन्सियां, फोड़े, एग्जिमा आदि अनेक स्वास्थ्यनाशक रोग मात्र मानसिक क्षोभ तथा भावनात्मक उद्देलन के परिणाम होते हैं।’’ मानसिक क्षोभ, भावनात्मक उद्देलन, निषेधात्मक चिन्तन, सूक्ष्म शरीर की विकृतियां हैं, जिनका स्थूल शरीर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार परिष्कृत दृष्टिकोण स्वस्थ-उदात्त चिन्तन, आदर्शवादी विचारधारा सूक्ष्म-शरीर को तेजस्वी प्रखर बनाती है और उसकी श्रेष्ठ प्रभाव स्थूल शरीर पर भी स्पष्ट देखा जा सकता है।
विधेयात्मक विचारों की, ऊर्ध्वमुखी चिन्तन की आश्चर्यजनक महत्ता के प्रतिपादन में डा. बैनेट ने स्वयं को ही प्रस्तुत किया है। 50 वर्ष की आयु तक डा. बैनेट निराशा और अवांछनीय चिन्तन के कारण अपना स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा बैठे। उन्हें जब ऊर्ध्वगामी चिन्तन की इस असीम उपादेयता का पता चला तो उन्होंने अपना जीवन क्रम ही बदल डाला। मन की जड़ता और विषय-विचारों का जुआ उनने उतार फेंका, हृदय को श्रद्धा आस्था से भरा, सदैव प्रसन्न प्रफुल्ल रहने की आदत बनाली। 20 वर्षों के अपने इस जीवन को स्वर्गीय सुख से ओत-प्रोत बनाते हुए डॉ. बैनेट ने अपनी 50 वर्षीय फोटो तथा 70 वर्षीय फोटो भी एक पुस्तक में छापी है। पहली में उनका चेहरा झुर्रियों से पिचके गाल, धंसी आंखों के कारण मनहूस दिखाई देता है जबकि 70 वर्ष की आयु में वे स्वस्थ सशक्त दिखाई देते हैं, झुर्रियां न जाने कहां चली गईं, चेहरे में उद्दीप्ति है और युवकों जैसी सक्रियता।
अब तक किये गये ऐसे ही विविध आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि मन का, मस्तिष्क का कष्ट प्रत्येक जीवाणु को कष्ट में डाल देता है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध का अनिष्ट प्रभाव समस्त जीवाणुओं में तुरन्त दौड़ जाता है, झलक उठता है। मस्तिष्क में प्रसन्नता का भाव आते ही प्रत्येक जीवाणु प्रसन्न-पुलकित हो उठता है। ये सभी जीवाणु परस्पर गहन आत्मीयता और अभिन्नता का भाव रखते हैं। प्रत्येक जीवाणु की दशा से सभी प्रभावित होते हैं—इनका सुख-दुःख मिला-जुला ही होता है। इनका पारस्परिक सौहार्द्र-सद्भावना अनूठा है। सच्ची मैत्री, प्रगाढ़ आत्मीयता समानुभूति के ये अनूठे उदाहरण हैं। कल्पना करें कि एक व्यक्ति को तेज भूख लगी है। सुस्वादु भोजन का थाल सामने है। उसी समय किसी प्रियजन की मृत्यु का तार मिलता है। उसे पढ़ते ही मस्तिष्क में उस प्रियजन की संचित स्मृति सहसा जागृत हो उठती है। मन में आत्मीय सम्वेदना उमड़ पड़ती है। मस्तिष्क के जीवाणुओं में हलचल, उथल-पुथल मच जाती है। मस्तिष्क के जीवाणुओं की इस प्रतिक्रिया का तत्काल सम्पूर्ण शरीर के जीवाणुओं पर प्रभाव पड़ता है। जीभ सूखने लगती है। भूख बढ़ाने वाले जीवाणु जो उछल-कूद मचा रहे थे, चीख-चीखकर भोजन की मांग कर रहे थे, सहमकर शान्त, निष्क्रिय, दुबके-से बैठ जाते हैं। हृदय और दूसरे अंग भी निष्प्राण से हो चलते हैं। दिल-डूबने लगता है, आंखों के सामने अन्धेरा छा जाता है, शरीर निढाल हो जाता है। समस्त अंगों पर यह प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि मस्तिष्कीय जीवाणुओं की भावदशा का तत्काल प्रभाव सम्पूर्ण शरीरस्थ जीवाणु-समूहों पर पड़ता है।
‘ओल्ड एज : इट्स काफ एन्ड प्रिवेन्शन’ नामक पुस्तक में उसके रचियता सुप्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक तथा लेखक डा. बैनेट ने एक बहुत ही मनोरंजक किन्तु शिक्षाप्रद घटना दी है। एक 19 वर्षीय फ्रान्सीसी युवती ने एक अमेरिकन नव-युवक से विवाह का निश्चय किया। युवक निर्धन था सो यह तय हुआ कि पहले वह अमेरिका जाकर धन कमायेगा और लौटकर शादी करेगा। युवक ने 3 वर्ष में पर्याप्त धन कमा लिया, पर दुर्भाग्य से कोई मुकदमा लग जाने के कारण वह 15 वर्ष तक फ्रान्स नहीं लौट सका। 15 वर्ष बाद जब वह वापस लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी मंगेतर का स्वास्थ्य, सौन्दर्य बिलकुल वैसा ही है जैसा वह 19 वर्ष पूर्व था। 34 वर्ष की अधेड़ अवस्था हो जाने पर उसमें 19 वर्षीय नव-युवती के गुण विद्यमान थे।
घटना का विवेचन करते हुये बैनेट महोदय लिखते हैं—प्रकृति ने मनुष्य शरीर की संचालन क्रिया प्रक्रिया इस प्रकार रखी है कि शरीर का प्रत्येक कोश (सैल) 80 दिन पीछे पुराना होकर मैल के रूप में उसी प्रकार बाहर निकल जाता है, जिस प्रकार समुद्री लहरों में निरन्तर ज्वार भाटे से समुद्र की गन्दगी तटों पर जमा होती रहती है। कोश-परिवर्तन की यह प्रक्रिया आयु बढ़ने के साथ क्षीण होती रहती है, उसी का नाम वृद्धावस्था है—किन्तु इस घटना ने इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही उलट दिया, ऐसा क्यों?
इसका उत्तर युवती के मुंह से दिलवाते हुये श्री बैनेट लिखते हैं कि—मैं प्रतिदिन प्रातःकाल एक आदमकद शीशे के सम्मुख खड़ी होकर अपना चेहरा देखती और मन की मन अनुभव करती की मैं ठीक वैसी ही हूं जैसी कल थी। दिन के परिवर्तन ने मेरे शरीर में कोई प्रभाव नहीं डाला इच्छा शक्ति की यह दृढ़ता मुझे दिन भर पुलकित और प्रसन्न बनाये रखती। उसी का फल है जो मैं जैसी 15 वर्ष पूर्व थी वैसी ही आज भी हूं।’’ सूक्ष्म शरीर के शोधन की विचारों को ऊंचा उठाने की संकल्प की महत्ता उन्होंने अमरीका के अध्यात्म परायण व्यक्ति डॉ. मारडन की पुस्तक ‘‘लौह इच्छा शक्ति’’ (ऐन आइरन विल) से समझी। जिसमें बताया गया है—‘‘मनुष्य अपने विचार नये करले, चरित्र को ऊंचा उठाले तो अपना शरीर ही बदल सकता है।’’ यह स्वाध्याय उनके लिये तो औषधि बना ही, सैकड़ों को नया जीवन देने वाला है। प्रेम, मैत्री, दया, करुणा और परोपकारी विचारों को धारण कर कोई भी इसका प्रत्यक्ष लाभ ले सकता है।
खोपड़ी के ऊपर या नीचे की रक्तवाहनियों की पेशियां भावनाओं के अनुसार फैलती-सिकुड़ती व तीव्र सम्वेदनात्मक प्रतिक्रियायें करती हैं।
अस्वस्थ भावनाएं विभिन्न शारीरिक रोगों का कारण बनती हैं। सामान्य सिर दर्द से लेकर ‘‘माइग्रेन’’ नामक कठिन सिर दर्द भावनात्मक तनाव से होता है। इस तनाव से खोपड़ी की रक्तवाहनियां सिकुड़ती हैं और इससे सिर दर्द शुरू हो जाता है। आज तो यह पाया जाता है कि सिर दर्द की सी घटनाओं में से पचासी का कारण भावनात्मक तनाव होता है।
भावना-क्षोभ के कारण पेशियों में उत्पन्न तनाव के कारण कई बार लोग भोजन के बाद ऐसा अनुभव करते हैं कि कलेजे पर बोझ आ पड़ा है और भोजन नीचे सरक ही नहीं रहा है। अधिक तनाव होने पर उबकाई आने लगती है, जी मिचलाने लगता है।
भावनात्मक तनाव से उत्पन्न स्नायु-रोगों में डकारें आना, पेट में ऐंठन होना, विभिन्न वायु-विकार अनेक त्वचा-विकार, एग्जिमा, खुजली आदि होते हैं।
कमर-दर्द के बारे में अब ऐसा ज्ञात हुआ है कि अधिकांश मामलों में इसका कारण भावनात्मक तनाव ही होता है। यह जान लेने पर कि भावनात्मक तनावों एवं विकृतियों से ही अधिकांश रोग पैदा होते हैं, यह प्रश्न अनेकों को कचोटता है कि भावनाओं पर नियन्त्रण कैसे हो? इसका एक ही सरल मार्ग है—समझदारी भरे दृष्टिकोण का नित्य-प्रति के जीवन में अभ्यास। बिना अभ्यास के यह दृष्टिकोण व्यावहारिक जीवन में नहीं उतरता। जिन्दगी को बोझ न मानते हुए खेल-भावना से जीना, अभ्यास द्वारा ही सम्भव है। अपनी सीमाओं को पहचानना, शक्ति के सर्वोत्तम उपयोग की व्यवस्था करना, ‘मैं-मैं’ की चीख-पुकार से मुक्त होकर अपने दायित्वों को समझना और निभाना, तथा सृजनात्मक वृत्तियों का जीवन में निरन्तर विकास करना ही एक मेध राजमार्ग है।
सामान्यतः कठोरता, क्रोध, बात-बात में लड़ बैठने आदि को हम भ्रान्तिवश शक्ति का पर्याय मान बैठते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक इस सबको ‘बचकानी हरकतें’ मानते हैं। ये दुर्बलता के प्रतीक हैं। शक्तिशाली व्यक्ति विनम्र एवं दृढ़ होता है। क्रोध और झगड़ालूपन तो शक्तिहीनता की उपज है। सादगी-संयम का अभ्यास ही शक्ति का स्रोत है। किन्तु अपनी दुर्बलताओं पर व्यर्थ की खीझ भी लाभकर न होगी। धीरे-धीरे ही कुसंस्कार चित तल पर जमते हैं और धीरे-धीरे ही उनका उन्मूलन सम्भव है। सतत् अभ्यास ही सर्वोत्तम उपचार है। इस बात को सदा ध्यान में रखा जाय कि मन की कुटिलता ओर अनैतिक कर्म ही रोग का आधार हैं तथा मन की शुचिता, स्नेह, करुणा और व्यापक मानवीय प्रेम द्वारा इन रोगों को मिटा सकना सरलता से सम्भव है।
मस्तिष्क की धुलाई-सफाई वैज्ञानिक उपकरणों से भी सम्भव हो सकती है। फिर अध्यात्म साधना के उपचार तो उससे अधिक ही सशक्त समर्थ होते हैं। उनका प्रभाव तो और भी अधिक होना चाहिये।
लेऐलेक्ट्रिकल स्टीम्यूलेशन आफ ब्रेन (ई.एस.बी.) पद्धति के अनुसार कई एशियन विश्वविद्यालयों ने आंशिक रूप से मस्तिष्क की धुलाई (ब्रेन वाशिंग) में सफलता प्राप्त करली है। अभी यह बन्दर, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे जैसे छोटे स्तर के जीवों पर ही प्रयोग किये गये हैं। आहार की रुचि, शत्रुता, मित्रता, भय, आक्रमण आदि आदि के सामान्य स्वभाव को जिस प्रकार चरितार्थ किया जाना चाहिए उसे वे बिलकुल भूल जाते हैं और विचित्र प्रकार का आचरण करते हैं। बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा गया तो वह आक्रमण करना तो दूर उससे डर कर एक कोने में जा छिपी। क्षणभर में एक-दूसरे पर खूनी आक्रमण करना, एक आध मिनट बाद परस्पर लिपट कर प्यार करना यह परिवर्तन उस विद्युत क्रिया से होता है जो उनके मस्तिष्कीय कोषों के साथ सम्बद्ध रहती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू हो सकती है। मानव मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत होता है उसमें प्रतिरोधक शक्ति भी अधिक होती है इसलिए उसमें हेर-फेर करने के लिए प्रयास भी कुछ अधिक करने पड़ेंगे और सफलता प्राप्त करने में देरी भी लगेगी, पर जो सिद्धांत स्पष्ट हो गये हैं उनके आधार पर यह निश्चित हो गया है कि मनुष्य को भी जैसा चाहे सोचने, मान्यता बनाने और गतिविधियां अपनाने के लिए विवश किया जा सकता है।
मनोमय कोश की साधना मस्तिष्कीय क्षेत्र की धुलाई सफाई ही नहीं करता, वरन् उसे समुन्नत सुसज्जित एवं सुसंस्कृत बनाने का काम भी बहुत हद तक पूरा कर सकती है। मनोमय कोश शरीर और मस्तिष्क के समूचे क्षेत्र को अपने अंचल में समेटे हुए हैं। वह इन दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अन्तःकरण के अस्त-व्यस्त और विकृत स्थिति से बने रहने पर उसकी प्रतिक्रिया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। व्यक्तित्व लड़खड़ा जाने पर दृष्टिकोण और व्यवहार दोनों ही गड़बड़ाते हैं। फलतः गतिविधियां अवांछनीयता से भर जाती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में विपत्तियां ही उत्पन्न होंगी। अवरोध ही खड़े होंगे। कलह और संकट आक्रमण करेंगे। समूचा जीवन ही नरक बन जायगा। इस नारकीय यन्त्रणा से छुटकारा कोई और नहीं दिला सकता। क्योंकि इस विपत्ति का दोष भले ही किसी पर थोपा जा सके उसका कारण अपना आपा ही होता है। मनःस्थिति के अनुरूप परिस्थिति बनने का तथ्य इतना स्पष्ट है कि उसे झुठलाये जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अपने आप में परिवर्तन किये बिना हम इस नरक से अन्य किसी तरह उबर नहीं सकते। जीवनक्रम में उत्पन्न विविध-विधि अवरोधों से छुटकारा पाये बिना हमारा उद्धार हो नहीं सकता। समस्याओं और विपन्नताओं से त्राण मिल नहीं सकता।
समृद्धि, प्रगति और सुख-शान्ति की समस्त सम्भावनायें बीज रूप में अपने ही भीतर भरी पड़ी हैं। सत्प्रवृत्तियों की देवी और सद्भावनाओं के देवता ही हमें दिव्य वरदानों से सुसम्पन्न बनाते हैं। अन्तरंग की विभूतियां ही बहिरंग की सिद्धियां बन कर सामने आती हैं। आत्मशोधन और आत्म परिष्कार जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। इसे प्रत्यक्ष कल्प-वृक्ष की उपमा दी जा सकती है।
मनोमय कोश का विज्ञान और साधन हमारी मानसिक स्थिति के परिष्कार का ऋषि प्रणीत उपाय है। इस दिशा में कदम बढ़ाने पर हम हर दृष्टि से लाभान्वित ही होते हैं।