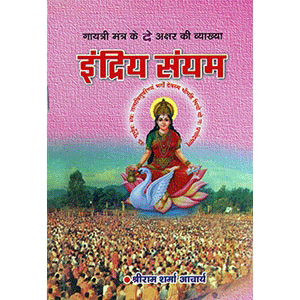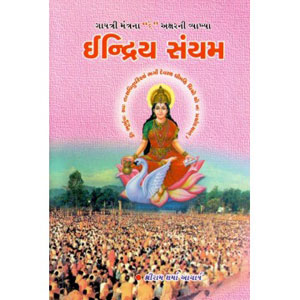इन्द्रिय संयम 
इन्द्रिय-संयम और ब्रह्मचर्य व्रत
Read Scan Version
ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा सर्व विदित है। इसकी शक्ति अमोघ मानी गई है, और आज संसार में जितने व्यक्तियों ने महान और उपयोगी काम कर दिखाये हैं वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के अनुगामी थे। जैसा अनेक बार बतलाया जा चुका है, ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि काम वृत्ति का सर्वथा परित्याग ही कर दिया जाये। उचित अवस्था प्राप्त होने पर शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उसको प्रयोग करना किसी ने बुरा नहीं बतलाया। इतना ही नहीं शास्त्रकारों ने तो उस गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी ही बतलाया है जो केवल अपनी स्त्री तक सीमित रहकर नियमानुकूल आचरण करता है।
ब्रह्मचर्य का विश्लेषण करने पर तीन तत्व मिलते हैं:—
(1) आत्मसंयम—ब्रह्मचर्य यथार्थ में शक्ति संयम ही है।
(2) सादगी—भोजन, वेश तथा जीवन के प्रत्येक अंग में; दैनिक जीवन की हरएक बात में सादगी रखना इसी की युवकों को जरूरत है। जो लोग जरूरतों के बढ़ाने को ही सभ्यता का अर्थ समझते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं, सच्ची सभ्यता सादगी में है, न कि संग्रह में।
(3) विचार शक्ति—ब्रह्मचर्य एक आन्तरिक शक्ति है। विचार शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है, सादगी का जीवन किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है, तथा आत्मसंयम या आत्मशक्ति किस प्रकार बढ़ सकती है इन बातों के विवेचन पर्याप्त किया जा चुका है; तो भी कुछ ऐसे साधन और अभ्यास हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य भाव की वृद्धि के लिए पालन करना आवश्यक है।
प्राचीन और आधुनिक में जो बड़ा भारी भेद है, वह है ब्रह्मचर्य और भोग का। वर्तमान आदर्शों के आन्तरिक महत्व को मैं नहीं भुलाता। आजकल के वैज्ञानिक विवेचन, आलोचनात्मक भाव तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावनाओं का मैं अनादर नहीं करता, किन्तु आधुनिक सभ्यता की इन आन्तरिक और गूढ़तर भावनाओं पर हमारी शालाओं में आजकल जोर नहीं दिया जाता। वहां तो आधुनिक सभ्यता के ऊपरी पहलू और गलत भावनाओं और दुर्गुणों ही पर दृष्टि रखी जाती है। नवयुवक भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि सभ्यता का अर्थ जरूरतों की बढ़ती या कामनाओं का संग्रह नहीं, किन्तु उनकी सादगी है। वे नहीं समझते कि मनुष्यता का नियम आत्मभोग नहीं, किन्तु आत्म-संयम है। प्राचीन भारत ने यह अनुभव किया था कि मनुष्य भोग विलासी जानवर नहीं, किन्तु वह एक दिव्य पुरुष है, जो कि आत्म-संयम और आत्म-तपस्या के द्वारा अपनी दिव्य मनुष्यता का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। प्राचीन आदर्श ब्रह्मचर्य था, वर्तमान आदर्श बहुतों की दृष्टि में भोगचर्य जान पड़ता है। वे आरामतलबी और विलासिता चाहते हैं, पर हिन्दू शास्त्रों के अनुसार तपस्या ही सभ्यता और सृष्टि की आधारशिला है।
अगर यह बात सही है, आहार का चारित्र्य पर इतना असर है तो विहार का याने लैंगिक शुद्धि का चारित्र्य पर कितना हो सकता है, इसका अनुमान करना कठिन नहीं होना चाहिये।
जिसे हम काम-विकार कहते हैं अथवा लैंगिक आकर्षण कहते हैं, वह केवल शारीरिक भावना नहीं है। मनुष्य के सारे के सारे पहलू उसमें उत्तेजित हो जाते हैं, और अपना-अपना काम करते हैं। इसलिए जिसमें शरीर, मन-हृदय की भावनायें और आत्मिक निष्ठा-सब का सहयोग अपरिहार्य है, ऐसी प्रवृत्ति का विचार एकांगी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। जीवन के सार्वभौम और सर्वोत्तम मूल्य से ही उसका विचार करना चाहिए। इस आचरण में शारीरिक प्रेरणा के वश होकर बाकी के सब तत्वों का अपमान किया जाता है, वह आचरण समाज-द्रोह तो करता ही है लेकिन उससे भी अधिक अपने व्यक्तित्व का महान द्रोह करता है।
लोग जिसे वैवाहिक प्रेम कहते हैं, उसके तीन पहलू हैं। एक भोग से सम्बन्ध रखता है, दूसरा प्रजा तन्तु से और तीसरा भावना की उत्कटता से। पहला प्रधानता शारीरिक है, दूसरा मुख्यतः सामाजिक और व्यापक अर्थ में आध्यात्मिक। यह तीसरा तत्व सब से महत्व का सार्वभौम है और उसी का असर जब पहले दोनों के ऊपर पूरा पूरा पड़ता है, तभी वे दोनों उत्कट, तृप्तिदायक और पवित्र बनते हैं।
इन तीन तत्वों में से पहला तत्व बिल्कुल पार्थिव होने से उसकी स्वाभाविक मर्यादायें भी होती हैं, भोग से शरीर क्षीण होता है। अति सेवन से भोग-शक्ति भी क्षीण होती है और भोग भी नीरस हो जाते हैं। भोग से संयम का प्रमाण जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक उसकी उत्कटता होगी। भोग में संयम का तत्व आने से ही उसमें आध्यात्मिकता आ सकती है। संयमपूर्ण भोग में ही निष्ठा और आध्यात्मिकता आकर टिक सकते हैं, और संयम और निष्ठा के बिना वैवाहिक जीवन का सामाजिक पहलू कृतार्थ हो ही नहीं सकता। केवल लाभ हानि की दृष्टि से देखा जाय तो वैवाहिक जीवन का परमोत्कर्ष संयम और अन्योन्य निष्ठा में ही है। भोग-तत्व पार्थिव हैं और इसलिए परमित हैं। भावना तत्व हार्दिक और आत्मिक होने से उसके विकास की कोई मर्यादा ही नहीं है।
आजकल के लोग जब कभी लैंगिक नीति की स्वच्छन्दता का प्रचार करते हैं, तब वे केवल भोग-प्रधान पार्थिव अंश को ही ध्यान में लेते हैं। जीवन की इतनी क्षुद्र कल्पना वे ले बैठे हैं कि थोड़े ही दिनों में उन्हें अनुभव हो जाता है कि ऐसी स्वतन्त्रता में किसी किस्म की सिद्धि नहीं है और न सच्ची तृप्ति। ऐसे लोगों ने अगर उच्च आदर्श ही छोड़ दिया तो फिर उनमें तारक असन्तोष भी नहीं बच पाता। विवाह-सम्बन्ध में केवल भोग के सम्बन्ध का विचार करने वाले लोगों ने भी अपना अनुभव जाहिर किया है—
संयम और निष्ठा ही सामाजिकता की सच्ची बुनियाद है। संयम से जो शक्ति पैदा होती है, वही चारित्र्य का आधार है। जो आदमी कहता है मैं संयम नहीं कर सकता, वह चारित्र्य की छोटी-मोटी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। इसलिए संयम ही चारित्र्य का मुख्य आधार है।
चारित्र्य का दूसरा आधार है निष्ठा। व्यक्ति के जीवन की कृतार्थता तभी हो सकती है, जब वह स्वतन्त्रता-पूर्वक समष्टि में विलीन हो जाता है। व्यक्ति स्वातन्त्र्य को सम्हालते हुए अगर समाज-परायणता सिद्ध करना हो तो वह अन्योन्य निष्ठा के बिना हो नहीं सकती और अखिल समाज के प्रति एक-सी अनन्य निष्ठा तभी सिद्ध होती है, जब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अथवा कम से कम वैवाहिक जीवन में परस्पर दृढ़ निष्ठा से प्रारम्भ करता है। अन्योन्य निष्ठा जब आदर्श कोटि तक पहुंचती है तब वहीं से सच्ची समाज-सेवा शुरू होती है।
अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि ‘मनके जीते जीत है, मनके हारे हार।’ अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया है और आप उस पर विवेक का अंकुश रखते हैं तो आपको संसार के व्यवहार करते हुए भी कोई कठिनाई प्रतीत न होगी। वैराग्य, त्याग, विरक्ति, इन महातत्वों का सीधा संबन्ध अपने मनोभावों से है। यदि भावनाएं संकीर्ण हों, कलुषित हों, स्वार्थमयी हों तो चाहे कैसी भी उत्तम सात्विक स्थिति में मनुष्य क्यों न रहे मनका विकार वहां भी पाप की, दुराचार की सृष्टि करेगा। यदि भावनाएं उदार एवं उत्तम हैं तो अनमिल और अनिष्ट कारक स्थिति में भी मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता उत्पन्न करेगा। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि—‘‘मुझे नरक में भेज दिया जाय तो भी मैं वहां अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा।’’ वास्तविक बात यही है कि बुराई-भलाई हमारे ही मन से उत्पन्न होती है। हमारी इन्द्रियां अगर बुरे मार्ग पर जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं, वरन् स्वयं मन पर ही है। अगर हमारा मन सुमार्गगामी रहकर इन्द्रियों को संयम में रखे तो समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुये भी हम सद्गति के अधिकारी बन सकते हैं।
ब्रह्मचर्य का विश्लेषण करने पर तीन तत्व मिलते हैं:—
(1) आत्मसंयम—ब्रह्मचर्य यथार्थ में शक्ति संयम ही है।
(2) सादगी—भोजन, वेश तथा जीवन के प्रत्येक अंग में; दैनिक जीवन की हरएक बात में सादगी रखना इसी की युवकों को जरूरत है। जो लोग जरूरतों के बढ़ाने को ही सभ्यता का अर्थ समझते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं, सच्ची सभ्यता सादगी में है, न कि संग्रह में।
(3) विचार शक्ति—ब्रह्मचर्य एक आन्तरिक शक्ति है। विचार शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है, सादगी का जीवन किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है, तथा आत्मसंयम या आत्मशक्ति किस प्रकार बढ़ सकती है इन बातों के विवेचन पर्याप्त किया जा चुका है; तो भी कुछ ऐसे साधन और अभ्यास हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य भाव की वृद्धि के लिए पालन करना आवश्यक है।
प्राचीन और आधुनिक में जो बड़ा भारी भेद है, वह है ब्रह्मचर्य और भोग का। वर्तमान आदर्शों के आन्तरिक महत्व को मैं नहीं भुलाता। आजकल के वैज्ञानिक विवेचन, आलोचनात्मक भाव तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावनाओं का मैं अनादर नहीं करता, किन्तु आधुनिक सभ्यता की इन आन्तरिक और गूढ़तर भावनाओं पर हमारी शालाओं में आजकल जोर नहीं दिया जाता। वहां तो आधुनिक सभ्यता के ऊपरी पहलू और गलत भावनाओं और दुर्गुणों ही पर दृष्टि रखी जाती है। नवयुवक भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि सभ्यता का अर्थ जरूरतों की बढ़ती या कामनाओं का संग्रह नहीं, किन्तु उनकी सादगी है। वे नहीं समझते कि मनुष्यता का नियम आत्मभोग नहीं, किन्तु आत्म-संयम है। प्राचीन भारत ने यह अनुभव किया था कि मनुष्य भोग विलासी जानवर नहीं, किन्तु वह एक दिव्य पुरुष है, जो कि आत्म-संयम और आत्म-तपस्या के द्वारा अपनी दिव्य मनुष्यता का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। प्राचीन आदर्श ब्रह्मचर्य था, वर्तमान आदर्श बहुतों की दृष्टि में भोगचर्य जान पड़ता है। वे आरामतलबी और विलासिता चाहते हैं, पर हिन्दू शास्त्रों के अनुसार तपस्या ही सभ्यता और सृष्टि की आधारशिला है।
संयम और सदाचार की महिमा
अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाने की साधना जिन्होंने की है, वे अनुभव से कहते आये हैं कि ‘आहारशुद्धो सत्वशुद्धिः’। इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि सत्व के दो माने हैं—शरीर का संगठन और चारित्र्य। अगर आहार शुद्ध है, याने स्वच्छ है, ताजा है, परिपक्व है, सुपाच्य है, प्रमाणयुक्त है और उसके घटक परम्परानुकूल हैं तो उसके सेवन से शरीर के रक्त, मज्जा, शुक्र आदि सब घटक शुद्ध होते हैं। वात, पित्त, कफ आदि की साम्यावस्था रहती है और सप्तधातु परिपुष्ट होकर शरीर सुदृढ़, कार्यक्षम तथा सब तरह के आघात सहन करने के योग्य बनता है और इस आरोग्य का मन पर भी अच्छा असर होता है। ‘आहारशुद्धो सत्वशुद्धिः’ का दूसरा और व्यापक अर्थ यह है कि आहार अगर प्रामाणिक है, हिंसाशून्य है, द्रोहशून्य है, और यज्ञ, दान, तप का फर्ज अदा करने के बाद प्राप्त किया गया है तो उससे चारित्र्य शुद्धि को पूरी पूरी मदद मिलती है। चारित्र्य शुद्धि का आधार ही इस प्रकार की आहार शुद्धि पर है।अगर यह बात सही है, आहार का चारित्र्य पर इतना असर है तो विहार का याने लैंगिक शुद्धि का चारित्र्य पर कितना हो सकता है, इसका अनुमान करना कठिन नहीं होना चाहिये।
जिसे हम काम-विकार कहते हैं अथवा लैंगिक आकर्षण कहते हैं, वह केवल शारीरिक भावना नहीं है। मनुष्य के सारे के सारे पहलू उसमें उत्तेजित हो जाते हैं, और अपना-अपना काम करते हैं। इसलिए जिसमें शरीर, मन-हृदय की भावनायें और आत्मिक निष्ठा-सब का सहयोग अपरिहार्य है, ऐसी प्रवृत्ति का विचार एकांगी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। जीवन के सार्वभौम और सर्वोत्तम मूल्य से ही उसका विचार करना चाहिए। इस आचरण में शारीरिक प्रेरणा के वश होकर बाकी के सब तत्वों का अपमान किया जाता है, वह आचरण समाज-द्रोह तो करता ही है लेकिन उससे भी अधिक अपने व्यक्तित्व का महान द्रोह करता है।
लोग जिसे वैवाहिक प्रेम कहते हैं, उसके तीन पहलू हैं। एक भोग से सम्बन्ध रखता है, दूसरा प्रजा तन्तु से और तीसरा भावना की उत्कटता से। पहला प्रधानता शारीरिक है, दूसरा मुख्यतः सामाजिक और व्यापक अर्थ में आध्यात्मिक। यह तीसरा तत्व सब से महत्व का सार्वभौम है और उसी का असर जब पहले दोनों के ऊपर पूरा पूरा पड़ता है, तभी वे दोनों उत्कट, तृप्तिदायक और पवित्र बनते हैं।
इन तीन तत्वों में से पहला तत्व बिल्कुल पार्थिव होने से उसकी स्वाभाविक मर्यादायें भी होती हैं, भोग से शरीर क्षीण होता है। अति सेवन से भोग-शक्ति भी क्षीण होती है और भोग भी नीरस हो जाते हैं। भोग से संयम का प्रमाण जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक उसकी उत्कटता होगी। भोग में संयम का तत्व आने से ही उसमें आध्यात्मिकता आ सकती है। संयमपूर्ण भोग में ही निष्ठा और आध्यात्मिकता आकर टिक सकते हैं, और संयम और निष्ठा के बिना वैवाहिक जीवन का सामाजिक पहलू कृतार्थ हो ही नहीं सकता। केवल लाभ हानि की दृष्टि से देखा जाय तो वैवाहिक जीवन का परमोत्कर्ष संयम और अन्योन्य निष्ठा में ही है। भोग-तत्व पार्थिव हैं और इसलिए परमित हैं। भावना तत्व हार्दिक और आत्मिक होने से उसके विकास की कोई मर्यादा ही नहीं है।
आजकल के लोग जब कभी लैंगिक नीति की स्वच्छन्दता का प्रचार करते हैं, तब वे केवल भोग-प्रधान पार्थिव अंश को ही ध्यान में लेते हैं। जीवन की इतनी क्षुद्र कल्पना वे ले बैठे हैं कि थोड़े ही दिनों में उन्हें अनुभव हो जाता है कि ऐसी स्वतन्त्रता में किसी किस्म की सिद्धि नहीं है और न सच्ची तृप्ति। ऐसे लोगों ने अगर उच्च आदर्श ही छोड़ दिया तो फिर उनमें तारक असन्तोष भी नहीं बच पाता। विवाह-सम्बन्ध में केवल भोग के सम्बन्ध का विचार करने वाले लोगों ने भी अपना अनुभव जाहिर किया है—
एतत्कामफल लोके यत् द्वयोः एकचित्तता ।
अन्य चित्तकृते कामे शवयो इव संगमः ।।
यह एकचित्तता यानी हृदय की एकता अथवा स्नेहग्रन्थि अन्योन्य निष्ठा और अपत्यनिष्ठा के बिना टिक ही नहीं सकती। बढ़ने की बात दूर रही।अन्य चित्तकृते कामे शवयो इव संगमः ।।
संयम और निष्ठा ही सामाजिकता की सच्ची बुनियाद है। संयम से जो शक्ति पैदा होती है, वही चारित्र्य का आधार है। जो आदमी कहता है मैं संयम नहीं कर सकता, वह चारित्र्य की छोटी-मोटी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। इसलिए संयम ही चारित्र्य का मुख्य आधार है।
चारित्र्य का दूसरा आधार है निष्ठा। व्यक्ति के जीवन की कृतार्थता तभी हो सकती है, जब वह स्वतन्त्रता-पूर्वक समष्टि में विलीन हो जाता है। व्यक्ति स्वातन्त्र्य को सम्हालते हुए अगर समाज-परायणता सिद्ध करना हो तो वह अन्योन्य निष्ठा के बिना हो नहीं सकती और अखिल समाज के प्रति एक-सी अनन्य निष्ठा तभी सिद्ध होती है, जब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अथवा कम से कम वैवाहिक जीवन में परस्पर दृढ़ निष्ठा से प्रारम्भ करता है। अन्योन्य निष्ठा जब आदर्श कोटि तक पहुंचती है तब वहीं से सच्ची समाज-सेवा शुरू होती है।
अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि ‘मनके जीते जीत है, मनके हारे हार।’ अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया है और आप उस पर विवेक का अंकुश रखते हैं तो आपको संसार के व्यवहार करते हुए भी कोई कठिनाई प्रतीत न होगी। वैराग्य, त्याग, विरक्ति, इन महातत्वों का सीधा संबन्ध अपने मनोभावों से है। यदि भावनाएं संकीर्ण हों, कलुषित हों, स्वार्थमयी हों तो चाहे कैसी भी उत्तम सात्विक स्थिति में मनुष्य क्यों न रहे मनका विकार वहां भी पाप की, दुराचार की सृष्टि करेगा। यदि भावनाएं उदार एवं उत्तम हैं तो अनमिल और अनिष्ट कारक स्थिति में भी मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता उत्पन्न करेगा। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि—‘‘मुझे नरक में भेज दिया जाय तो भी मैं वहां अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा।’’ वास्तविक बात यही है कि बुराई-भलाई हमारे ही मन से उत्पन्न होती है। हमारी इन्द्रियां अगर बुरे मार्ग पर जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं, वरन् स्वयं मन पर ही है। अगर हमारा मन सुमार्गगामी रहकर इन्द्रियों को संयम में रखे तो समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुये भी हम सद्गति के अधिकारी बन सकते हैं।
***
*समाप्त*
*समाप्त*