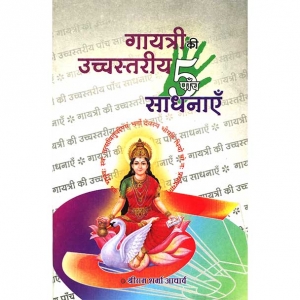गायत्री की उच्चस्तरीय पाँच साधनाएँ 
खेचरी मुद्रा की प्रतिक्रिया और उपलब्धि
Read Scan Version
उच्चस्तरीय साधनाओं में खेचरी मुद्रा को रसानुभूति का, दिव्य आनन्द का मूल स्रोत माना गया है। यह मुख्यतया जीभ और तालु गह्वर की साधना है। इस साधना में लम्बी जिह्वा का बड़ा महत्व होता है इसीलिए खेचरी मुद्रा की साधना के लिये हठयोगी जीभ को लम्बी करके ‘काक चंचु’ तक पहुंचाने के लिये जिह्वा पर काली मिर्च, शहद, घृत का लेपन करके उसे थन की तरह दुहते, खींचते हैं और लम्बी करने का प्रयत्न करते हैं। जीभ के नीचे वाली पतली त्वचा को काट कर भी अधिक पीछे तक मुड़ सकने योग्य उसे बनाया जाता है। यह दोनों ही क्रियायें सर्वसाधारण के उपयुक्त नहीं हैं। इनमें तनिक भी भूल होने से जिह्वा तन्त्र ही नष्ट हो सकता है अथवा दूसरी विपत्तियां आ सकती हैं। अस्तु यदि सर्वजनीन एवं जोखिम रहित उपासनाएं अभीष्ट हों तो शारीरिक अवयवों पर अनावश्यक दबाव न डालकर सारी प्रक्रिया को ध्यान परक—भावना मूलक ही रखना होगा।
खेचरी मुद्रा का भावपक्ष ही वस्तुतः उस प्रक्रिया का प्राण है। मस्तिष्क मध्य को—ब्रह्मरंध्र अवस्थित सहस्रार को—अमृत-कलश माना गया है और वहां से सोमरस स्रवित होते रहने का उल्लेख है। जिह्वा को जितना सरलतापूर्वक पीछे तालु से सटाकर जितना पीछे ले जा सकना सम्भव हो उतना पीछे ले जाना चाहिए। ‘काक चंचु’ से बिलकुल न सट सके कुछ फासले पर रह जावे तो भी हर्ज नहीं है। तालु और जिह्वा को इस प्रकार सटाने के उपरान्त ध्यान किया जाना चाहिए कि तालु छिद्र से अमृत का— सूक्ष्म स्राव टपकता है और जिह्वा इन्द्रिय के गहन अन्तराल में रहने वाली रस तन्मात्रा द्वारा उसका पान किया जा रहा है। इसी सम्वेदना को अमृत पान पर सोमरस पान की अनुभूति कहते हैं। प्रत्यक्षतः कोई मीठी वस्तु खाने आदि जैसा कोई स्वाद तो नहीं आता, पर कई प्रकार के दिव्य रसास्वादन उस अवसर पर हो सकते हैं। यह इन्द्रिय अनुभूतियां मिलती हो तो हर्ज नहीं, पर वे आवश्यक या अनिवार्य नहीं हैं। मुख्य तो वह भावपक्ष है जो इस आस्वादन के बहाने गहन रस सम्वेदना से सिक्त रहता है। यही आनन्द और उल्लास की अनुभूति-खेचरी मुद्रा की मूल उपलब्धि है।
देवी भागवत पुराण में महाशक्ति की वन्दना करते हुए उसे कुण्डलिनी और खेचरी मुद्रा से सम्बन्धित बताया गया है— तालुस्था त्वं सदाधारा विंदुस्था विंदुमालिंनी । मूले कुण्डलीशक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा ।। —देवी भागवत
अमृतधारा सोम सावित्री खेचरी रूप तालु में, भ्रूमध्य भाग आज्ञा चक्र में बिन्दु माला और मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी बनकर आप ही निवास करती है और प्रत्येक रोम कूप में विद्यमान है।
शिव संहिता में प्रसुप्त कुण्डलिनी का जागरण करने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास आवश्यक बताते हुए कहा गया है— तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधपितुमीश्वरीम् । ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत् ।। —शिव संहिता
इसलिए साधक को ब्रह्मरन्ध्र के मुख में, रास्ता रोके सोती पड़ी कुण्डलिनी के जागृत करने के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए और खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए।
कभी-कभी खेचरी मुद्रा के अभ्यास काल में कई प्रकार के रसों के आस्वादन जैसी झलक भी मिलती है। कई बार रोमांच जैसा होने लगता है, पर यह सब आवश्यक या अनिवार्य नहीं मूल उद्देश्य तो भावानुभूति ही है।
अमृतास्वादनं पश्चाज्जिह्वाग्रे संप्रवर्तते । रोमांचश्च तथानन्दः प्रकर्षेणोपजायते ।। —योग रसायनम् 255
जिह्वाग्र में अमृत-सा सुस्वाद अनुभव होता है और रोमांच तथा आनन्द उत्पन्न होता है। प्रथमं लवणं पश्चात् क्षारं क्षीरोपमं ततः । द्राक्षारससमं पश्चात् सुधासारमयं ततः ।। —योग रसायनम्
खेचरी मुद्रा के समय उस रस का स्वाद पहले लवण जैसा, फिर क्षार जैसा, फिर दूध जैसा, फिर द्राक्षारस जैसा और तदुपरान्त अनुपम सुधा, रस-सा अनुभव होता है।
आदौ लवण क्षारं च ततस्तिक्त कषायकम् । नवनीतं घृतं क्षीरं दधित क्रम धूनि च । द्राक्षा रसं च पीयूषं जायते रसनोदकम् । —घेरण्ड संहिता
खेचरी मुद्रा में जिह्वा को क्रमशः नमक, क्षार, तिक्त, कषाय, नवनीत, घृत, दूध, दही, द्राक्षारस, पीयूष, जल जैसे रसों की अनुभूति होती है।
अमृतास्वादनाद्देहो योगिनो दिव्यतामियात् । जरारोगविनिर्मुक्तश्चिर जीवति भूतले ।। —योग रसायनम्
भावनात्मक अमृतोपम स्वाद मिलने पर योगी के शरीर में दिव्यता आ जाती है और वह रोग तथा जीर्णता से मुक्त होकर दीर्घकाल तक जीवित रहता है।
एक योग सूत्र में खेचरी मुद्रा से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति का उल्लेख है—
तालु मूलोर्ध्वभागे महज्ज्योति विद्यते तद्दर्शनाद् अणिमादि सिद्धिः । तालु के ऊर्ध्व भाग में महा ज्योति है, उसके दर्शन से अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। घेरण्ड संहिता में खेचरी मुद्रा का प्रतिफल इस प्रकार बताया गया है—
न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैव लस्य प्रजायत । न च रोगो जरा मृत्युर्देव देहः स जायते ।।
खेचरी मुद्रा की निष्णात देव देह का मूर्च्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, रोग, जरा, मृत्यु का भय नहीं रहता।
लावण्यं च भवेद्गात्रे समाधि जयिते ध्रुवम् । कपाल वक्त्र संयोगे रसना रस माप्नुयात् ।। —घेरण्ड.
शरीर सौन्दर्यवान बनता है। समाधि का आनन्द मिलता है रसों की अनुभूति होती है। खेचरी मुद्रा सब प्रकार श्रेयस्कर है।
जरामृत्युगदघ्नो यः खेचरी वेत्ति भूतले । ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव तदभ्यास प्रयोगतः ।। तं मुने सर्वभावेन गुरु गत्वा समाश्रयेत् । —योगकुण्डल्युपनिषद
जो महापुरुष ग्रन्थ से, अर्थ से और अभ्यास-प्रयोग से इस जरा मृत्यु व्याधि-निवारक खेचरी विद्या को जानने वाला है, उसी गुरु के पास सर्वभाव से आश्रय ग्रहण कर इस विद्या का अभ्यास करना चाहिए।
खेचरी मुद्रा से अनेकों शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक लाभों के उपलब्ध होने का शास्त्रों में वर्णन है। इससे सामान्य दीखने वाली इस महान साधना का महत्व समझा जा सकता है। स्मरणीय इतना ही है कि इस मुद्रा के साथ-साथ भाव सम्वेदनाओं की अनुभूति अधिकतम गहरी एवं श्रद्धा सिक्त होनी चाहिए। जिह्वा को उलट कर तालु से लगाना और अनुभव करना कि इसके ऊपर सहस्रार अमृत कलश से रिस-रिस कर टपकने वाले सोमरस का जिह्वाग्र भाग से पान किया जा रहा है—यही खेचरी मुद्रा है। तालु में मधुमक्खियों के छत्ते जैसे कोष्टक होते हैं। सहस्रार को शतदल, सहस्रदल-कमल की उपमा दी गई है। तालु सहस्र धारा है। उसके कोष्टक शरीर शास्त्र की दृष्टि से उच्चारण एवं भोजन चबाने, निगलने आदि के कार्यों में सहायता करते हैं। योगशास्त्र की दृष्टि से उनसे दिव्य स्राव निसृत होते हैं। ब्रह्म चेतना मानवी सम्पर्क में आते समय सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में अवतरित होती है। इसके बाद वहां मनुष्य की स्थिति, आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप काया के विभिन्न अवयवों में चली जाती है। शेष अंश अन्तरिक्ष में विलीन हो जाता है।
जिह्वा को तालु से स्पर्श कराने के कई उद्देश्य हैं। मुख गह्वर में रहने वाली रसेन्द्रिय, रयिशक्ति सम्पन्न—ऋण विद्युत सदृश होती है। उसे मुखर कुण्डलिनी कहते हैं सर्पिणी की तुलना भी उस पर सही रीति से लागू होती है। अनगढ़ कुसंस्कारी प्रसुप्त स्थिति में वह स्वाद के नाम पर कुछ भी—कितना ही—बिना विवेक के खाती है। पेट को दुर्बल और रक्त को विषाक्त करती है। फलतः दुर्बलता और अस्वस्थता की चक्की में पिसते हुये आधा-अधूरा कष्ट पूर्ण जीवन जी सकना सम्भव होता है। शेष तो अकाल मृत्यु की तरह आत्म-हत्या की तरह ही नष्ट होता है। यह सर्पिणी के काटने सदृश ही दुखदायी है। इसी प्रकार जिह्वा द्वारा कटु वचन, हेय परामर्श, छल-प्रपंच आदि द्वारा अपने को गर्हित अधःपतित और दूसरों को कुमार्ग अपनाने के लिये उत्तेजित किया जाता है। यह भी सर्पिणी का ही काम है। द्रौपदी की जीभ ने महाभारत की पृष्ठभूमि बनाई थी, यह सर्वविदित है। यह अनगढ़ प्रसुप्त—स्थिति हुई। यदि यह जिह्वा कुण्डलिनी जागृत हो सके—सुसंस्कृत बन सके तो आहार संयम के लिए जागरूक रहती है। बोलते समय प्रिय और हित का अमृत घोलती है। फलतः सम्भाषणकर्ती को श्रेय एवं सम्मान की अजस्र उपलब्धियां होती हैं। सुसंस्कृत जिह्वा के अनुदानों ने कितनों को न जाने किन-किन वरदानों से लाद दिया है। प्रामाणिक और सुसंस्कृत वक्तता के आधार पर ही तो लोग अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व करते और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचे दिखाई पड़ते हैं। ऐसी ही अन्य विशेषताओं के कारण जिह्वा को मुखर कुण्डलिनी कहा गया है और मुख को ऊर्ध्व मूलाधार बताया गया है। निम्न मूलाधार में कामबीज का और ऊर्ध्व मूलाधार मुख में—ज्ञान बीज का निर्झर झरता है। जननेन्द्रियों की और मुख की आकृति को समतुल्य बताना—कहने-सुनने में तो भोंड़ा लगता है, पर योगशास्त्र की दृष्टि से दोनों की वस्तुस्थिति में बहुत कुछ समानता है। इन्द्रियों में कामुकता और स्वादेन्द्रिय यह दो ही प्रधान मानी गई हैं। संयम साधना में जिह्वा का संयम होने पर कामेन्द्रिय का संयम सहज ही सध जाने की बात नितान्त तथ्यपूर्ण है। इसमें दोनों के बीच की घनिष्ठता प्रत्यक्ष है। काम क्रीड़ा में भी यह दोनों ही गह्वर अपने-अपने ढंग से उत्तेजित रहते और अपना-अपना पक्ष पूरा करते हैं।
जिह्वा में ऋण विद्युत की प्रधानता है। मस्तिष्क धन विद्युत का केन्द्र है। तालु मस्तिष्क की ही निचली परत है। जिह्वा को भावना पूर्ण तालु से लगाने पर आत्मरति जैसा उद्देश्य पूरा होता है। जिह्वा और तालू की हलकी भावना पूर्ण रगड़ से एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक स्पन्दन आरम्भ होते हैं। उनसे उत्पन्न उत्तेजना से ब्रह्मानन्द की अनुभूति का लाभ मिलता है। यह सूक्ष्म होने के कारण कायिक विषयानन्द से अत्यन्त उच्चकोटि का कहा गया है। इस अनुभूति को योगीजन अमृत निर्झर का रसास्वादन कहते हैं।
खेचरी मुद्रा की साधना ब्रह्मलोक से—ब्रह्मरंध्र से—सामीप्य साधती है और उस केन्द्र के अनुदानों को उसी प्रकार चूसती है जैसे छोटे बालक का मुख माता का स्तन चूसता है। यह भावना एवं कल्पना सूक्ष्म शरीर में एक विशेष प्रकार की सुखद एवं उत्साहवर्धक गुदगुदी उत्पन्न करती है। उसका रसास्वादन देर तक करते रहने को जी करता है। यह तो हुआ भावनात्मक पथ जिससे अन्तःचेतना के अमृत से सम्पर्क बनता है और अन्तर्मुखी होकर अन्तर्जगत में एक से एक बढ़ी-बढ़ी दिव्य सम्वेदनाओं की अनुभूति का द्वार खुलता है। पर बात इतने तक ही सीमित नहीं है। जिह्वा की ‘ऋण’ विद्युत ब्रह्मलोक से—ब्रह्मरंध्र से अन्यान्य अनुदानों की सम्पदा के ‘धन’ भण्डार को अपने चुम्बकत्व से खींचती, घसीटती है और उसकी मात्रा बढ़ाते-बढ़ाते अपने अन्तः भण्डार को दिव्य विभूतियों से भरती चली जाती है। इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये खेचरी मुद्रा के द्वारा उत्पन्न लाभों का सुविस्तृत वर्णन योग ग्रन्थों में लिखा और अनुभवियों द्वारा बताया मिलता है।
तालु और जिह्वा के हलके संस्पर्श स्थिर नहीं, वरन् हलकी रगड़ जैसे होते रहते हैं। इसमें घड़ी के पेंडुलम जैसी गति बनती है। गाय को दुहते समय भी इसी से मिलती-जुलती क्रिया-पद्धति कार्यान्वित होती है। रति कर्म की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की है। रगड़ से ऊर्जा का—हलचल का—उत्पन्न होना सर्वविदित है। यह ऊर्जा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को प्रभावित करती है। उन्हें बल देती—सक्रिय करती और समर्थ बनाती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोशों के अनावरण में इससे सहायता मिलती है। षट्चक्रों को जागृत करने में भी खेचरी मुद्रा से उत्पन्न ऊर्जा की एक बड़ी भूमिका रहती है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए कुण्डलिनी जागरण में खेचरी मुद्रा को महत्व दिया गया है। क्रिया साधारण-सी होते हुए भी प्रतिक्रिया की दृष्टि से उसका बहुत ऊंचा स्थान माना गया है। अचेतन के साथ सम्बन्धित अतीन्द्रिय ज्ञान के विकास विस्तार में उससे असाधारण सहायता मिलती है।
परमात्मा का आत्मा के साथ निरन्तर पेंडुलम गति से ही मिलन सम्पर्क चलता रहता है। इस संस्पर्श की अनुभूति (1) आनन्द और (2) उल्लास के रूप में होती रहती है। सामान्य स्थिति में तो इसकी प्रतीत नहीं होती पर खेचरी मुद्रा के माध्यम से उसे अनुभव किया जा सकता है। भगवान की मनुष्य को दो प्रेरणाएं हैं जो उपलब्ध हैं, उसकी गरिमा को समझते हुए संसार के सुखद पक्ष का मूल्यांकन करते हुए—सन्तुष्ट, प्रसन्न और आनन्दित रहना यह है आनन्द का स्वरूप। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व की दिशा में साहस भरे कदम उठाने के लिये अदम्य उत्साह का—भावभरी उमंगों का उठना यह है उल्लास। भगवान इन्हीं दो प्रेरणाओं को निरन्तर पेण्डुलम गति से प्रदान करते रहते हैं। मानव जीवन जैसी सृष्टि की अनुपम उपलब्धि को पाकर यदि अंतःकरण आनन्दित रहे और छोटे-मोटे अभावों की ओर अधिक ध्यान न देकर चारों ओर बिखरी हुई सदाशयता का अनुभव करते हुये सन्तुष्ट सन्तुलित रहे तो समझना चाहिये आनन्द की उपलब्धि हो रही है। हर्षातिरेक में उछलने-कूदने या बढ़-चढ़कर शेखीखोरी की बातें करने का नाम आनन्द नहीं है। उस स्थिति में दृष्टिकोण परिपक्व हो जाता है और परिष्कृत, इसलिये जिन अभावों और असफलताओं में दूसरे लोग उद्विग्न उत्तेजित हो उठते हैं, उन्हें वह विनोद कौतुक भर समझते हुए अपनी मनःस्थिति को सुसन्तुलित बनाये रहता है। जिनकी मनोभूमि ऐसी हो उसे आनन्द की प्राप्ति हो गई ऐसा कहा जा सकता है।
आनन्दित, सन्तुष्ट या प्रसन्न होने में एक दोष यह है कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने के लिए जिस कठोर कर्मठता की जरूरत पड़ती है उसे प्रायः भुला दिया जाता है। ऐसी भूल करने वाले अध्यात्मवादी प्रायः निकम्मे, अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी और बुराइयों, बुरी परिस्थितियों से समझौता कर लेने वाले, भाग्यवादी, पलायनवादी बन बैठते हैं। उनसे उनकी अपनी समग्र प्रगति का द्वार तो बन्द हो ही जाता है, साथ ही समाज के लिए प्रखर कर्त्तव्य-पालन के लिए जो महान् उत्तरदायित्व मनुष्य के कन्धों पर होते हैं वे भी अवरुद्ध हो जाने से लोकमंगल के लिए मानवी योगदान में भी भारी क्षति पहुंचती है। मनुष्य का अवतरण जिन महान् कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का प्रचण्ड प्रयत्नशीलता के साथ निर्वाह करने के लिए हुआ, यदि उनमें शिथिलता आ गई तो समझना चाहिए कि जीवित ही मृतक बन जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि आनन्द या सन्तोष की प्राप्ति किसी अध्यात्मवादी में इस प्रकार की अकर्मण्यता उत्पन्न करदे तो समझना चाहिए कि बिलकुल उलटा हो गया और अर्थ का अनर्थ बन गया। खेचरी मुद्रा की साधना से उपलब्ध होने वाला दूसरा दिव्य अनुदान उल्लास माना गया है। यह उभरता उल्लास इस प्रकार की अवांछनीय मनःस्थिति बनने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। भगवान निरन्तर आनन्द के साथ-साथ उल्लास भी प्रदान करते हैं और उच्चस्तरीय प्रयत्नों के लिए प्रचण्ड कर्मठता अपनाने के लिए अदम्य स्फूर्ति एवं उमंग उत्पन्न करते हैं। उल्लास जब अपनी प्रौढ़ावस्था में होता है तो वह इतना प्रखर होता है कि प्रस्तुत कठिनाइयों, अभावों, अवरोधों की चिन्ता न करते हुए ईश्वरीय सन्देश के अनुरूप अपनी रीति-नीति निर्धारित करने के लिए मचल उठता है। किसी के रोके नहीं रुकता। लोभ और मोह के भव-बन्धन यों सहज नहीं टूटते और कुसंस्कार तथा स्वार्थ सम्बन्धी शुभचिन्तक ऐसी भावनाओं को क्रियान्वित होने में पग-पग पर विरोध उत्पन्न करते हैं, पर जिसे उल्लास प्राप्त है वह आत्म-कल्याण और ईश्वरीय निर्देशों के पालन की दिशा में ही अग्रसर होता है। कठिनाइयां क्यों आती हैं और रोकथाम कौन-कौन करते हैं इसकी चिन्ता नहीं करता। फलस्वरूप जहां चाह वहां राह वाली बात बन ही जाती है। जिसे उल्लास की उपलब्धि मिल गई उसे महापुरुषों जैसे महान् कर्त्तव्य-पालन करते रहने के अनवरत अवसर निर्वाध गति से मिलते ही रहते हैं।
आनन्द और उल्लास भरी मनःस्थिति उत्पन्न करने में खेचरी मुद्रा का जो योगदान मिलता है उसके फलस्वरूप साधक को हर स्थिति में हंसते-हंसाते रहने और हलकी फुलकी जिन्दगी जीने का अभ्यास करना पड़ता है। कर्मठता की जागरूकता से सामान्य जीवन-क्रम में पग-पग पर सफलताएं मिलती और सरलताएं उत्पन्न होती हैं। इन लाभों को भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मलोक के अन्य दिव्य अनुदान पाकर तो मानवी सत्ता ऋषिकल्प-देवतुल्य बनने के लिए अग्रसर होती है। खेचरी मुद्रा का वह विशिष्ट लाभ भी आनन्द उल्लास की उपलब्धि की तरह है, साधक के लिए हर दृष्टि से श्रेयस्कर सिद्ध होता है।
उच्चस्तरीय साधनाओं में तीसरा स्थान शक्तिचालनी मुद्रा का है। कुण्डलिनी जागरण में मूलाधार से प्रसुप्त कुण्डलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। उस महाशक्ति की सामान्य प्रवृत्ति अधोगामी रहती है। रतिक्रिया में उसका स्खलन होता रहता है। शरीर यात्रा की मल-मूत्र विसर्जन प्रक्रिया भी स्वभावतः अधोगामी है। शुक्र का क्षण भी इसी दिशा में होता है। इस प्रकार यह सारा संस्थान अधोगामी प्रवृत्तियों में संलग्न रहता है।
कुण्डलिनी शक्ति के जागरण और उत्थान के लिए इस क्षेत्र को ऊर्ध्वगामी बनने का अभ्यास कराया जाता है। ताकि अभीष्ट उद्देश्य की सफलता में सहायता मिल सके। गुदा मार्ग को ऊर्ध्वगामी अभ्यास कराने के लिए हठयोग में ‘वस्ति क्रिया’ है। उसमें गुदा द्वार से जल को ऊपर खींचा जाता है फिर संचित मल को बाहर निकाला जाता है। इसी क्रिया को ‘वस्ति’ कहते हैं। इसी प्रकार मूत्र मार्ग से जल ऊपर खींचने और फिर विसर्जित करने की क्रिया वज्रोली कहलाती है। वस्ति और वज्रोली दोनों का ही उद्देश्य इन विसर्जन छिद्रों को अधोमुखी अभ्यासों के साथ ही ऊर्ध्वगामी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अभ्यासों से कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायता मिलती है।
वस्ति और वज्रोली काफी कठिन हैं। हठयोग की साधनाएं सर्व-सुलभ नहीं हैं। उन्हें विशेष मार्गदर्शन से विशेष व्यक्ति ही कर सकते हैं। उन अभ्यासों में समय भी बहुत लगता है और भूल होने पर संकट उत्पन्न होने का खतरा भी रहता है। अस्तु सर्वजनीन सरलीकरण का ध्यान रखते हुए ‘शक्तिचालनी मुद्रा’ को उपयुक्त समझा गया है। शक्ति चालनी मुद्रा में गुदा और मूत्र संस्थान का संकल्प बल के सहारे संकोचन कराया जाता है। संकोचन का तात्पर्य है उनकी बहिर्मुखी एवं अधोगामी आदत को अंतर्मुखी एवं ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। इसके लिए दोनों ही इन्द्रियों का—उसके सुविस्तृत क्षेत्र का संकोचन कराया जाता है। कभी-कभी मुंह से हवा खींची जाती है, पानी पिया जाता है। इसमें मुख को खींचने की क्रिया करनी पड़ती है। पिचकारी में पानी भरते समय भी ऐसा ही होता है। मल और मूत्र छिद्रों से ऐसा ही वायु खींचने का, छोड़ने का, खींचने छोड़ने का प्राणायाम जैसा अभ्यास करना संक्षेप में शक्तिचालनी मुद्रा का प्रयोग है।
इस प्रयोग का पूर्वार्ध मूलबंध कहलाता है। मूलबन्ध में मात्र संकोचन भर होता है। जितनी देर मल-मूत्र छिद्रों को सिकोड़ा जाता रहेगा उतनी देर मूलबन्ध की स्थिति मानी जाएगी। यह एक पक्ष है। आधा अभ्यास है। इसमें पूर्णता समग्रता तब आती है जब प्राणायाम की तरह खींचने छोड़ने के दोनों ही अंग पूरे होने लगें। जब संकोचन-विसर्जन, संकोचन-विसर्जन का—खींचने ढीला करने, खींचने ढीला करने का—उभय पक्षीय अभ्यास चल पड़े तो समझना चाहिए शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास हो रहा है। कमर से नीचे के भाग में अपान वायु रहता है। उसे ऊपर खींचकर कमर से ऊपर रहने वाली प्राणवायु के साथ जोड़ा जाता है। यह पूर्वार्ध हुआ। उत्तरार्ध में ऊपर के प्राण को नीचे के अपान के साथ जोड़ा जाता है। यह प्राण अपान के संयोग की योग शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है—यही मूलबंध है। इस साधना की महिमा बताते हुए कहा गया है—
आकुंचनेन तं प्राहुर्मू लबंधोऽयमुच्यते । अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वन्हिना सह गच्छति ।। —योग कुण्डल्योपनिषद्
मूलबन्ध के अभ्यास से अधोगामी अपान को बलात् ऊर्ध्वगामी बनाया जाय, इससे वह प्रदीप्त होकर अग्नि के साथ-साथ ही ऊपर चढ़ता है।
अभ्यासाद् बन्धनस्यास्य मरुत् सिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् । साधयेद् यत्नतो तर्हि मौनी तु विजितालसः ।। (घेरण्डसंहिता 3।17)
मूलबन्ध के अभ्यास से मरुत् सिद्धि होती है अर्थात् शरीरस्थ वायु पर नियन्त्रण होता है। अतः अलस्य-विहीन होकर मौन रहते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए।
प्राणापानौ नादबिन्दु मूलबन्धेन चैकताम् । गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः ।। —हठयोग प्रदीपिका
प्राण और अपान का समागम-नाद बिंदु की साधना तथा मूलबन्ध का समन्वय, यह कर लेने पर निश्चित रूप से योग की सिद्धि होती है।
अपान प्राणयो रैक्यं क्षयोमूल पुरीष्योः । युवाभवति वृद्धोऽपि सतनं मूलबन्धनात् ।। —हठयोग प्रदीपिका
निरन्तर मूलबन्ध का अभ्यास करने से प्राण और अपान के समन्वय से—अनावश्यक मल नष्ट होते हैं और वृद्धता भी यौवन में बदलती है।
विलं प्रविष्टेव ततो व्रह्नाह्यंतरं व्रजेत् । तस्मान्नित्यं मूलबंधः कर्तव्यो योगिभिः सदा । —हठयोग प्र.
मूलबन्ध से कुण्डलिनी का प्रवेश ब्रह्मनाड़ी—सुषुम्ना—में होता है। इसलिए योगीजन नित्य ही मूलबन्ध का अभ्यास करें।
सिद्वये सर्वं भूतानि विश्वाधिष्ठानमद्वयम् । यस्मिन सिद्धिं गताः निद्धास्तासिद्धासनमुच्यते ।। यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम् । मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योउसौ ब्रह्मवादिनाम् ।। —तेजबिन्दु.
जो सर्वलोकों का मूल है। जो चित्त निरोध का मूल है, सो यह आत्मा ही ब्रह्मवादियों को सदा सेवन करना चाहिए। यही मूलबन्ध है। अन्यजुदा संकोचन रूप मूलबन्ध जिज्ञासुओं के लिए सेव्य नहीं है।
विलं प्रविष्टे ततो ब्रह्मनाडयन्तरं व्रजेत् । तस्मा न्नित्यं मूलबंधः कर्तव्यो योगिभिः सदा ।। —हठयोग प्रदीपिका 3।69
फिर जिस प्रकार सर्पिणी बिल में प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उद्दीप्त कुण्डलिनी ब्रह्मनाड़ी में प्रविष्ट होती है। इसीलिए योगियों को सदा ही मूलबन्ध का अभ्यास करना चाहिये।
मूलबन्ध एवं शक्तिचालिनी मुद्रा को विशिष्ट प्राणायाम कहा जा सकता है। सामान्य प्राणायाम में नासिका से सांस खींचकर प्राण प्रवाह को नीचे मूलाधार तक ले जाने और फिर ऊपर की ओर उसे वापिस लेकर नासिका द्वार से निकालते हैं। यही प्राण संचरण की क्रिया जब अधोभाग के माध्यम से की जाती है तो मूलबन्ध कहलाती है। नासिका का तो स्वभाव सांसें लेते और छोड़ते रहना है। अतः उसके साथ प्राण संचार का क्रम सुविधापूर्वक चल पड़ता है। गुदा अथवा उपस्थ इन्द्रियों द्वारा वायु खींचने जैसी कोई क्रिया नहीं होती अतः उस क्षेत्र के स्नायु संस्थान पर खिंचाव पैदा करके सीधे ही प्राण संचार का अभ्यास करना पड़ता है। प्रारम्भ में थोड़ा अस्वाभाविक लगता है किन्तु क्रमशः अभ्यास में आ जाता है।
मूलबन्ध में सुखासन, (सामान्य पालथी मार कर बैठना) पद्मासन (पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठना) सिद्धासन (मल-मूत्र छिद्रों के मध्य भाग पर एड़ी का दबाव डालना) इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
मल-द्वार को धीरे-धीरे सिकोड़ा जाय और ऐसा प्रयत्न किया जाय कि उस मार्ग से वायु खींचने के लिए संकोचन क्रिया की जा रही है। मल का वेग अत्यधिक हो और तत्काल शौच जाने का अवसर न हो तो उसे रोकने के लिए मल मार्ग को सिकोड़ने और ऊपर खींचने जैसी चेष्टा करनी पड़ती है। ऐसा ही मूलबन्ध में भी किया जाता है। मल द्वार को ही नहीं उस सारे क्षेत्र को सिकोड़ने का ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि मानो वायु अथवा जल को उस छिद्र से खींच रहे हैं। वज्रोली क्रिया में मूत्र मार्ग से पिचकारी की तरह जल ऊपर खींचने और फिर निकाल देने का अभ्यास किया जाता है। मूलबन्ध में जल आदि खींचने की बात तो नहीं है, पर संकल्प बल से गुदा द्वार ही नहीं मूत्र छिद्र से भी वायु खींचने जैसा प्रयत्न किया जाता है और उस सारे क्षेत्र को ऊपर खींचने का प्रयास चलता है गुदा मार्ग से वायु खींचकर नाभि से ऊपर तक घसीट ले जाने की चेष्टा आरम्भिक है। कुछ अधिक समय तक रुकना संभव होता है तो अपान को नाभि से ऊपर हृदय तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। यह खींचने का ऊपर ले जाने का पूर्वार्ध हुआ।
उत्तरार्ध में प्राणवायु को नाभि से नीचे की ओर लाया जाता है और अपान अपनी जगह आ जाता है। इसका व्यावहारिक स्वरूप यह है कि खींचने सिकोड़ने की क्रिया को ढीला छोड़ने, नीचे उतारने, खाली करने का वैसा ही प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि प्राणायाम में रेचन के लिये सांस छोड़ी जाती है।
मोटेतौर से उसे गुदा मार्ग को, मूत्र मार्ग को ऊपर की ओर सिकोड़ने की—पूरा संकोचन हो जाने पर कुछ देर रोके रहने की अन्ततः उसे ढीला छोड़ देने की गुदा मार्ग से होने वाली प्राणायाम क्रिया कहा जा सकता है।
स्मरण रहे कि यह क्रिया वायु संचार की नहीं प्राण संचार की है। नासिका द्वारा तो वायु संचार क्रम चलता ही रहता है, अतः उसके साथ प्राण प्रक्रिया जोड़ने में कठिनाई नहीं होती। मूलाधार क्षेत्र में श्वास लेने जैसा अभ्यास किसी इन्द्रिय को नहीं है, किन्तु प्राण संचार की क्षमता उस क्षेत्र में ऊर्ध्वभाग से किसी भी प्रकार कम नहीं। मूलबन्ध द्वारा प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाना प्रथम चरण है। दूसरे चरण में शक्तिचालनी मुद्रा के अभ्यास से प्राण, अपान आदि शरीरस्थ प्राणों को इच्छानुसार समुचित अनुपात में एक-दूसरे से जोड़ा, मिलाया जाना सम्भव होता है। ऐसा करने से शरीरस्थ पंच प्राण महाप्राण से संबद्ध हो जाते हैं।
गीता में योग साधक द्वारा प्राण को अपान में तथा अपान को प्राण में होमने का उल्लेख इसी दृष्टि से किया गया है। यथा :—
अपाने जुह्वति प्राणः प्राणोऽपान तथा परे । प्राणवान गतिं रूद्ववा प्राणायाम परायणाः ।।
अर्थात्—कोई साधक अपान में प्राण को आहुति देते हैं, कुछ प्राण में अपान को होमते हैं। प्राण और अपान की गति नियन्त्रित करके साधक प्राणायाम परायण होता है। नासिका द्वारा प्राण संचार करके उसे मूलाधार तक ले जाना प्राण को अपान में होमना है, और मूलबन्ध एवं शक्तिचालिनी मुद्रा आदि द्वारा ‘अपान’ का उत्थान करके उसे प्राण से मिलाना—अपान को प्राण में होमना कहा जाता है। प्राण और अपान दोनों की ही सामान्य गति को नियन्त्रित करके उसे उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना ही प्राणायाम का उद्देश्य है।
शक्तिचालनी मुद्रा का महत्व एवं लाभ योग शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है—
शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचारेत् । आयुर्वृद्धिर्भवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम् ।। —शिवसंहिता
शक्तिशालिनी मुद्रा का प्रतिदिन जो अभ्यास करता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है।
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता । सा शक्तिश्चालिता येन संयुक्तो नात्र सशयः ।। —हठयोग प्रदीपिका
कुण्डलिनी सर्पिणी की तरह कुटिल है, उसे शक्तिचालनी मुद्रा द्वारा जो चलायमान कर लेता है वही योगी है।
शक्तिचालन की महत्ता में जो कुछ कहा गया है वह अतिशयोक्ति नहीं। यह विज्ञान सम्मत है। शक्ति कहीं से आती नहीं, सुप्त से जागृत, जड़ से चलायमान हो जाना ही शक्ति का विकास कहा जाता है। बिजली के जनरेटर में बिजली कहीं से आती नहीं है। चुम्बकीय क्षेत्र में सुक्वायल घुमाने से उसके अन्दर के इलेक्ट्रॉन विशेष दिशा में चल पड़ते हैं। यह चलने की प्रवृत्ति विद्युत संवाहक शक्ति (ई.एम.एफ.) के रूप में देखी जाती है। शरीरस्थ विद्युत को भी इसी प्रकार दिशा विशेष में प्रवाहित किया जा सके तो शरीर संस्थान एक सशक्त जेनरेटर की तरह सक्षम एवं समर्थ बन सकता है। योग साधनायें इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।
खेचरी मुद्रा का भावपक्ष ही वस्तुतः उस प्रक्रिया का प्राण है। मस्तिष्क मध्य को—ब्रह्मरंध्र अवस्थित सहस्रार को—अमृत-कलश माना गया है और वहां से सोमरस स्रवित होते रहने का उल्लेख है। जिह्वा को जितना सरलतापूर्वक पीछे तालु से सटाकर जितना पीछे ले जा सकना सम्भव हो उतना पीछे ले जाना चाहिए। ‘काक चंचु’ से बिलकुल न सट सके कुछ फासले पर रह जावे तो भी हर्ज नहीं है। तालु और जिह्वा को इस प्रकार सटाने के उपरान्त ध्यान किया जाना चाहिए कि तालु छिद्र से अमृत का— सूक्ष्म स्राव टपकता है और जिह्वा इन्द्रिय के गहन अन्तराल में रहने वाली रस तन्मात्रा द्वारा उसका पान किया जा रहा है। इसी सम्वेदना को अमृत पान पर सोमरस पान की अनुभूति कहते हैं। प्रत्यक्षतः कोई मीठी वस्तु खाने आदि जैसा कोई स्वाद तो नहीं आता, पर कई प्रकार के दिव्य रसास्वादन उस अवसर पर हो सकते हैं। यह इन्द्रिय अनुभूतियां मिलती हो तो हर्ज नहीं, पर वे आवश्यक या अनिवार्य नहीं हैं। मुख्य तो वह भावपक्ष है जो इस आस्वादन के बहाने गहन रस सम्वेदना से सिक्त रहता है। यही आनन्द और उल्लास की अनुभूति-खेचरी मुद्रा की मूल उपलब्धि है।
देवी भागवत पुराण में महाशक्ति की वन्दना करते हुए उसे कुण्डलिनी और खेचरी मुद्रा से सम्बन्धित बताया गया है— तालुस्था त्वं सदाधारा विंदुस्था विंदुमालिंनी । मूले कुण्डलीशक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा ।। —देवी भागवत
अमृतधारा सोम सावित्री खेचरी रूप तालु में, भ्रूमध्य भाग आज्ञा चक्र में बिन्दु माला और मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी बनकर आप ही निवास करती है और प्रत्येक रोम कूप में विद्यमान है।
शिव संहिता में प्रसुप्त कुण्डलिनी का जागरण करने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास आवश्यक बताते हुए कहा गया है— तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधपितुमीश्वरीम् । ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत् ।। —शिव संहिता
इसलिए साधक को ब्रह्मरन्ध्र के मुख में, रास्ता रोके सोती पड़ी कुण्डलिनी के जागृत करने के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए और खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए।
कभी-कभी खेचरी मुद्रा के अभ्यास काल में कई प्रकार के रसों के आस्वादन जैसी झलक भी मिलती है। कई बार रोमांच जैसा होने लगता है, पर यह सब आवश्यक या अनिवार्य नहीं मूल उद्देश्य तो भावानुभूति ही है।
अमृतास्वादनं पश्चाज्जिह्वाग्रे संप्रवर्तते । रोमांचश्च तथानन्दः प्रकर्षेणोपजायते ।। —योग रसायनम् 255
जिह्वाग्र में अमृत-सा सुस्वाद अनुभव होता है और रोमांच तथा आनन्द उत्पन्न होता है। प्रथमं लवणं पश्चात् क्षारं क्षीरोपमं ततः । द्राक्षारससमं पश्चात् सुधासारमयं ततः ।। —योग रसायनम्
खेचरी मुद्रा के समय उस रस का स्वाद पहले लवण जैसा, फिर क्षार जैसा, फिर दूध जैसा, फिर द्राक्षारस जैसा और तदुपरान्त अनुपम सुधा, रस-सा अनुभव होता है।
आदौ लवण क्षारं च ततस्तिक्त कषायकम् । नवनीतं घृतं क्षीरं दधित क्रम धूनि च । द्राक्षा रसं च पीयूषं जायते रसनोदकम् । —घेरण्ड संहिता
खेचरी मुद्रा में जिह्वा को क्रमशः नमक, क्षार, तिक्त, कषाय, नवनीत, घृत, दूध, दही, द्राक्षारस, पीयूष, जल जैसे रसों की अनुभूति होती है।
अमृतास्वादनाद्देहो योगिनो दिव्यतामियात् । जरारोगविनिर्मुक्तश्चिर जीवति भूतले ।। —योग रसायनम्
भावनात्मक अमृतोपम स्वाद मिलने पर योगी के शरीर में दिव्यता आ जाती है और वह रोग तथा जीर्णता से मुक्त होकर दीर्घकाल तक जीवित रहता है।
एक योग सूत्र में खेचरी मुद्रा से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति का उल्लेख है—
तालु मूलोर्ध्वभागे महज्ज्योति विद्यते तद्दर्शनाद् अणिमादि सिद्धिः । तालु के ऊर्ध्व भाग में महा ज्योति है, उसके दर्शन से अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। घेरण्ड संहिता में खेचरी मुद्रा का प्रतिफल इस प्रकार बताया गया है—
न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैव लस्य प्रजायत । न च रोगो जरा मृत्युर्देव देहः स जायते ।।
खेचरी मुद्रा की निष्णात देव देह का मूर्च्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, रोग, जरा, मृत्यु का भय नहीं रहता।
लावण्यं च भवेद्गात्रे समाधि जयिते ध्रुवम् । कपाल वक्त्र संयोगे रसना रस माप्नुयात् ।। —घेरण्ड.
शरीर सौन्दर्यवान बनता है। समाधि का आनन्द मिलता है रसों की अनुभूति होती है। खेचरी मुद्रा सब प्रकार श्रेयस्कर है।
जरामृत्युगदघ्नो यः खेचरी वेत्ति भूतले । ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव तदभ्यास प्रयोगतः ।। तं मुने सर्वभावेन गुरु गत्वा समाश्रयेत् । —योगकुण्डल्युपनिषद
जो महापुरुष ग्रन्थ से, अर्थ से और अभ्यास-प्रयोग से इस जरा मृत्यु व्याधि-निवारक खेचरी विद्या को जानने वाला है, उसी गुरु के पास सर्वभाव से आश्रय ग्रहण कर इस विद्या का अभ्यास करना चाहिए।
खेचरी मुद्रा से अनेकों शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक लाभों के उपलब्ध होने का शास्त्रों में वर्णन है। इससे सामान्य दीखने वाली इस महान साधना का महत्व समझा जा सकता है। स्मरणीय इतना ही है कि इस मुद्रा के साथ-साथ भाव सम्वेदनाओं की अनुभूति अधिकतम गहरी एवं श्रद्धा सिक्त होनी चाहिए। जिह्वा को उलट कर तालु से लगाना और अनुभव करना कि इसके ऊपर सहस्रार अमृत कलश से रिस-रिस कर टपकने वाले सोमरस का जिह्वाग्र भाग से पान किया जा रहा है—यही खेचरी मुद्रा है। तालु में मधुमक्खियों के छत्ते जैसे कोष्टक होते हैं। सहस्रार को शतदल, सहस्रदल-कमल की उपमा दी गई है। तालु सहस्र धारा है। उसके कोष्टक शरीर शास्त्र की दृष्टि से उच्चारण एवं भोजन चबाने, निगलने आदि के कार्यों में सहायता करते हैं। योगशास्त्र की दृष्टि से उनसे दिव्य स्राव निसृत होते हैं। ब्रह्म चेतना मानवी सम्पर्क में आते समय सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में अवतरित होती है। इसके बाद वहां मनुष्य की स्थिति, आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप काया के विभिन्न अवयवों में चली जाती है। शेष अंश अन्तरिक्ष में विलीन हो जाता है।
जिह्वा को तालु से स्पर्श कराने के कई उद्देश्य हैं। मुख गह्वर में रहने वाली रसेन्द्रिय, रयिशक्ति सम्पन्न—ऋण विद्युत सदृश होती है। उसे मुखर कुण्डलिनी कहते हैं सर्पिणी की तुलना भी उस पर सही रीति से लागू होती है। अनगढ़ कुसंस्कारी प्रसुप्त स्थिति में वह स्वाद के नाम पर कुछ भी—कितना ही—बिना विवेक के खाती है। पेट को दुर्बल और रक्त को विषाक्त करती है। फलतः दुर्बलता और अस्वस्थता की चक्की में पिसते हुये आधा-अधूरा कष्ट पूर्ण जीवन जी सकना सम्भव होता है। शेष तो अकाल मृत्यु की तरह आत्म-हत्या की तरह ही नष्ट होता है। यह सर्पिणी के काटने सदृश ही दुखदायी है। इसी प्रकार जिह्वा द्वारा कटु वचन, हेय परामर्श, छल-प्रपंच आदि द्वारा अपने को गर्हित अधःपतित और दूसरों को कुमार्ग अपनाने के लिये उत्तेजित किया जाता है। यह भी सर्पिणी का ही काम है। द्रौपदी की जीभ ने महाभारत की पृष्ठभूमि बनाई थी, यह सर्वविदित है। यह अनगढ़ प्रसुप्त—स्थिति हुई। यदि यह जिह्वा कुण्डलिनी जागृत हो सके—सुसंस्कृत बन सके तो आहार संयम के लिए जागरूक रहती है। बोलते समय प्रिय और हित का अमृत घोलती है। फलतः सम्भाषणकर्ती को श्रेय एवं सम्मान की अजस्र उपलब्धियां होती हैं। सुसंस्कृत जिह्वा के अनुदानों ने कितनों को न जाने किन-किन वरदानों से लाद दिया है। प्रामाणिक और सुसंस्कृत वक्तता के आधार पर ही तो लोग अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व करते और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचे दिखाई पड़ते हैं। ऐसी ही अन्य विशेषताओं के कारण जिह्वा को मुखर कुण्डलिनी कहा गया है और मुख को ऊर्ध्व मूलाधार बताया गया है। निम्न मूलाधार में कामबीज का और ऊर्ध्व मूलाधार मुख में—ज्ञान बीज का निर्झर झरता है। जननेन्द्रियों की और मुख की आकृति को समतुल्य बताना—कहने-सुनने में तो भोंड़ा लगता है, पर योगशास्त्र की दृष्टि से दोनों की वस्तुस्थिति में बहुत कुछ समानता है। इन्द्रियों में कामुकता और स्वादेन्द्रिय यह दो ही प्रधान मानी गई हैं। संयम साधना में जिह्वा का संयम होने पर कामेन्द्रिय का संयम सहज ही सध जाने की बात नितान्त तथ्यपूर्ण है। इसमें दोनों के बीच की घनिष्ठता प्रत्यक्ष है। काम क्रीड़ा में भी यह दोनों ही गह्वर अपने-अपने ढंग से उत्तेजित रहते और अपना-अपना पक्ष पूरा करते हैं।
जिह्वा में ऋण विद्युत की प्रधानता है। मस्तिष्क धन विद्युत का केन्द्र है। तालु मस्तिष्क की ही निचली परत है। जिह्वा को भावना पूर्ण तालु से लगाने पर आत्मरति जैसा उद्देश्य पूरा होता है। जिह्वा और तालू की हलकी भावना पूर्ण रगड़ से एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक स्पन्दन आरम्भ होते हैं। उनसे उत्पन्न उत्तेजना से ब्रह्मानन्द की अनुभूति का लाभ मिलता है। यह सूक्ष्म होने के कारण कायिक विषयानन्द से अत्यन्त उच्चकोटि का कहा गया है। इस अनुभूति को योगीजन अमृत निर्झर का रसास्वादन कहते हैं।
खेचरी मुद्रा की साधना ब्रह्मलोक से—ब्रह्मरंध्र से—सामीप्य साधती है और उस केन्द्र के अनुदानों को उसी प्रकार चूसती है जैसे छोटे बालक का मुख माता का स्तन चूसता है। यह भावना एवं कल्पना सूक्ष्म शरीर में एक विशेष प्रकार की सुखद एवं उत्साहवर्धक गुदगुदी उत्पन्न करती है। उसका रसास्वादन देर तक करते रहने को जी करता है। यह तो हुआ भावनात्मक पथ जिससे अन्तःचेतना के अमृत से सम्पर्क बनता है और अन्तर्मुखी होकर अन्तर्जगत में एक से एक बढ़ी-बढ़ी दिव्य सम्वेदनाओं की अनुभूति का द्वार खुलता है। पर बात इतने तक ही सीमित नहीं है। जिह्वा की ‘ऋण’ विद्युत ब्रह्मलोक से—ब्रह्मरंध्र से अन्यान्य अनुदानों की सम्पदा के ‘धन’ भण्डार को अपने चुम्बकत्व से खींचती, घसीटती है और उसकी मात्रा बढ़ाते-बढ़ाते अपने अन्तः भण्डार को दिव्य विभूतियों से भरती चली जाती है। इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये खेचरी मुद्रा के द्वारा उत्पन्न लाभों का सुविस्तृत वर्णन योग ग्रन्थों में लिखा और अनुभवियों द्वारा बताया मिलता है।
तालु और जिह्वा के हलके संस्पर्श स्थिर नहीं, वरन् हलकी रगड़ जैसे होते रहते हैं। इसमें घड़ी के पेंडुलम जैसी गति बनती है। गाय को दुहते समय भी इसी से मिलती-जुलती क्रिया-पद्धति कार्यान्वित होती है। रति कर्म की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की है। रगड़ से ऊर्जा का—हलचल का—उत्पन्न होना सर्वविदित है। यह ऊर्जा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को प्रभावित करती है। उन्हें बल देती—सक्रिय करती और समर्थ बनाती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोशों के अनावरण में इससे सहायता मिलती है। षट्चक्रों को जागृत करने में भी खेचरी मुद्रा से उत्पन्न ऊर्जा की एक बड़ी भूमिका रहती है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए कुण्डलिनी जागरण में खेचरी मुद्रा को महत्व दिया गया है। क्रिया साधारण-सी होते हुए भी प्रतिक्रिया की दृष्टि से उसका बहुत ऊंचा स्थान माना गया है। अचेतन के साथ सम्बन्धित अतीन्द्रिय ज्ञान के विकास विस्तार में उससे असाधारण सहायता मिलती है।
परमात्मा का आत्मा के साथ निरन्तर पेंडुलम गति से ही मिलन सम्पर्क चलता रहता है। इस संस्पर्श की अनुभूति (1) आनन्द और (2) उल्लास के रूप में होती रहती है। सामान्य स्थिति में तो इसकी प्रतीत नहीं होती पर खेचरी मुद्रा के माध्यम से उसे अनुभव किया जा सकता है। भगवान की मनुष्य को दो प्रेरणाएं हैं जो उपलब्ध हैं, उसकी गरिमा को समझते हुए संसार के सुखद पक्ष का मूल्यांकन करते हुए—सन्तुष्ट, प्रसन्न और आनन्दित रहना यह है आनन्द का स्वरूप। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व की दिशा में साहस भरे कदम उठाने के लिये अदम्य उत्साह का—भावभरी उमंगों का उठना यह है उल्लास। भगवान इन्हीं दो प्रेरणाओं को निरन्तर पेण्डुलम गति से प्रदान करते रहते हैं। मानव जीवन जैसी सृष्टि की अनुपम उपलब्धि को पाकर यदि अंतःकरण आनन्दित रहे और छोटे-मोटे अभावों की ओर अधिक ध्यान न देकर चारों ओर बिखरी हुई सदाशयता का अनुभव करते हुये सन्तुष्ट सन्तुलित रहे तो समझना चाहिये आनन्द की उपलब्धि हो रही है। हर्षातिरेक में उछलने-कूदने या बढ़-चढ़कर शेखीखोरी की बातें करने का नाम आनन्द नहीं है। उस स्थिति में दृष्टिकोण परिपक्व हो जाता है और परिष्कृत, इसलिये जिन अभावों और असफलताओं में दूसरे लोग उद्विग्न उत्तेजित हो उठते हैं, उन्हें वह विनोद कौतुक भर समझते हुए अपनी मनःस्थिति को सुसन्तुलित बनाये रहता है। जिनकी मनोभूमि ऐसी हो उसे आनन्द की प्राप्ति हो गई ऐसा कहा जा सकता है।
आनन्दित, सन्तुष्ट या प्रसन्न होने में एक दोष यह है कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने के लिए जिस कठोर कर्मठता की जरूरत पड़ती है उसे प्रायः भुला दिया जाता है। ऐसी भूल करने वाले अध्यात्मवादी प्रायः निकम्मे, अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी और बुराइयों, बुरी परिस्थितियों से समझौता कर लेने वाले, भाग्यवादी, पलायनवादी बन बैठते हैं। उनसे उनकी अपनी समग्र प्रगति का द्वार तो बन्द हो ही जाता है, साथ ही समाज के लिए प्रखर कर्त्तव्य-पालन के लिए जो महान् उत्तरदायित्व मनुष्य के कन्धों पर होते हैं वे भी अवरुद्ध हो जाने से लोकमंगल के लिए मानवी योगदान में भी भारी क्षति पहुंचती है। मनुष्य का अवतरण जिन महान् कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का प्रचण्ड प्रयत्नशीलता के साथ निर्वाह करने के लिए हुआ, यदि उनमें शिथिलता आ गई तो समझना चाहिए कि जीवित ही मृतक बन जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि आनन्द या सन्तोष की प्राप्ति किसी अध्यात्मवादी में इस प्रकार की अकर्मण्यता उत्पन्न करदे तो समझना चाहिए कि बिलकुल उलटा हो गया और अर्थ का अनर्थ बन गया। खेचरी मुद्रा की साधना से उपलब्ध होने वाला दूसरा दिव्य अनुदान उल्लास माना गया है। यह उभरता उल्लास इस प्रकार की अवांछनीय मनःस्थिति बनने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। भगवान निरन्तर आनन्द के साथ-साथ उल्लास भी प्रदान करते हैं और उच्चस्तरीय प्रयत्नों के लिए प्रचण्ड कर्मठता अपनाने के लिए अदम्य स्फूर्ति एवं उमंग उत्पन्न करते हैं। उल्लास जब अपनी प्रौढ़ावस्था में होता है तो वह इतना प्रखर होता है कि प्रस्तुत कठिनाइयों, अभावों, अवरोधों की चिन्ता न करते हुए ईश्वरीय सन्देश के अनुरूप अपनी रीति-नीति निर्धारित करने के लिए मचल उठता है। किसी के रोके नहीं रुकता। लोभ और मोह के भव-बन्धन यों सहज नहीं टूटते और कुसंस्कार तथा स्वार्थ सम्बन्धी शुभचिन्तक ऐसी भावनाओं को क्रियान्वित होने में पग-पग पर विरोध उत्पन्न करते हैं, पर जिसे उल्लास प्राप्त है वह आत्म-कल्याण और ईश्वरीय निर्देशों के पालन की दिशा में ही अग्रसर होता है। कठिनाइयां क्यों आती हैं और रोकथाम कौन-कौन करते हैं इसकी चिन्ता नहीं करता। फलस्वरूप जहां चाह वहां राह वाली बात बन ही जाती है। जिसे उल्लास की उपलब्धि मिल गई उसे महापुरुषों जैसे महान् कर्त्तव्य-पालन करते रहने के अनवरत अवसर निर्वाध गति से मिलते ही रहते हैं।
आनन्द और उल्लास भरी मनःस्थिति उत्पन्न करने में खेचरी मुद्रा का जो योगदान मिलता है उसके फलस्वरूप साधक को हर स्थिति में हंसते-हंसाते रहने और हलकी फुलकी जिन्दगी जीने का अभ्यास करना पड़ता है। कर्मठता की जागरूकता से सामान्य जीवन-क्रम में पग-पग पर सफलताएं मिलती और सरलताएं उत्पन्न होती हैं। इन लाभों को भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मलोक के अन्य दिव्य अनुदान पाकर तो मानवी सत्ता ऋषिकल्प-देवतुल्य बनने के लिए अग्रसर होती है। खेचरी मुद्रा का वह विशिष्ट लाभ भी आनन्द उल्लास की उपलब्धि की तरह है, साधक के लिए हर दृष्टि से श्रेयस्कर सिद्ध होता है।
उच्चस्तरीय साधनाओं में तीसरा स्थान शक्तिचालनी मुद्रा का है। कुण्डलिनी जागरण में मूलाधार से प्रसुप्त कुण्डलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। उस महाशक्ति की सामान्य प्रवृत्ति अधोगामी रहती है। रतिक्रिया में उसका स्खलन होता रहता है। शरीर यात्रा की मल-मूत्र विसर्जन प्रक्रिया भी स्वभावतः अधोगामी है। शुक्र का क्षण भी इसी दिशा में होता है। इस प्रकार यह सारा संस्थान अधोगामी प्रवृत्तियों में संलग्न रहता है।
कुण्डलिनी शक्ति के जागरण और उत्थान के लिए इस क्षेत्र को ऊर्ध्वगामी बनने का अभ्यास कराया जाता है। ताकि अभीष्ट उद्देश्य की सफलता में सहायता मिल सके। गुदा मार्ग को ऊर्ध्वगामी अभ्यास कराने के लिए हठयोग में ‘वस्ति क्रिया’ है। उसमें गुदा द्वार से जल को ऊपर खींचा जाता है फिर संचित मल को बाहर निकाला जाता है। इसी क्रिया को ‘वस्ति’ कहते हैं। इसी प्रकार मूत्र मार्ग से जल ऊपर खींचने और फिर विसर्जित करने की क्रिया वज्रोली कहलाती है। वस्ति और वज्रोली दोनों का ही उद्देश्य इन विसर्जन छिद्रों को अधोमुखी अभ्यासों के साथ ही ऊर्ध्वगामी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन अभ्यासों से कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायता मिलती है।
वस्ति और वज्रोली काफी कठिन हैं। हठयोग की साधनाएं सर्व-सुलभ नहीं हैं। उन्हें विशेष मार्गदर्शन से विशेष व्यक्ति ही कर सकते हैं। उन अभ्यासों में समय भी बहुत लगता है और भूल होने पर संकट उत्पन्न होने का खतरा भी रहता है। अस्तु सर्वजनीन सरलीकरण का ध्यान रखते हुए ‘शक्तिचालनी मुद्रा’ को उपयुक्त समझा गया है। शक्ति चालनी मुद्रा में गुदा और मूत्र संस्थान का संकल्प बल के सहारे संकोचन कराया जाता है। संकोचन का तात्पर्य है उनकी बहिर्मुखी एवं अधोगामी आदत को अंतर्मुखी एवं ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। इसके लिए दोनों ही इन्द्रियों का—उसके सुविस्तृत क्षेत्र का संकोचन कराया जाता है। कभी-कभी मुंह से हवा खींची जाती है, पानी पिया जाता है। इसमें मुख को खींचने की क्रिया करनी पड़ती है। पिचकारी में पानी भरते समय भी ऐसा ही होता है। मल और मूत्र छिद्रों से ऐसा ही वायु खींचने का, छोड़ने का, खींचने छोड़ने का प्राणायाम जैसा अभ्यास करना संक्षेप में शक्तिचालनी मुद्रा का प्रयोग है।
इस प्रयोग का पूर्वार्ध मूलबंध कहलाता है। मूलबन्ध में मात्र संकोचन भर होता है। जितनी देर मल-मूत्र छिद्रों को सिकोड़ा जाता रहेगा उतनी देर मूलबन्ध की स्थिति मानी जाएगी। यह एक पक्ष है। आधा अभ्यास है। इसमें पूर्णता समग्रता तब आती है जब प्राणायाम की तरह खींचने छोड़ने के दोनों ही अंग पूरे होने लगें। जब संकोचन-विसर्जन, संकोचन-विसर्जन का—खींचने ढीला करने, खींचने ढीला करने का—उभय पक्षीय अभ्यास चल पड़े तो समझना चाहिए शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास हो रहा है। कमर से नीचे के भाग में अपान वायु रहता है। उसे ऊपर खींचकर कमर से ऊपर रहने वाली प्राणवायु के साथ जोड़ा जाता है। यह पूर्वार्ध हुआ। उत्तरार्ध में ऊपर के प्राण को नीचे के अपान के साथ जोड़ा जाता है। यह प्राण अपान के संयोग की योग शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है—यही मूलबंध है। इस साधना की महिमा बताते हुए कहा गया है—
आकुंचनेन तं प्राहुर्मू लबंधोऽयमुच्यते । अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वन्हिना सह गच्छति ।। —योग कुण्डल्योपनिषद्
मूलबन्ध के अभ्यास से अधोगामी अपान को बलात् ऊर्ध्वगामी बनाया जाय, इससे वह प्रदीप्त होकर अग्नि के साथ-साथ ही ऊपर चढ़ता है।
अभ्यासाद् बन्धनस्यास्य मरुत् सिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् । साधयेद् यत्नतो तर्हि मौनी तु विजितालसः ।। (घेरण्डसंहिता 3।17)
मूलबन्ध के अभ्यास से मरुत् सिद्धि होती है अर्थात् शरीरस्थ वायु पर नियन्त्रण होता है। अतः अलस्य-विहीन होकर मौन रहते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए।
प्राणापानौ नादबिन्दु मूलबन्धेन चैकताम् । गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः ।। —हठयोग प्रदीपिका
प्राण और अपान का समागम-नाद बिंदु की साधना तथा मूलबन्ध का समन्वय, यह कर लेने पर निश्चित रूप से योग की सिद्धि होती है।
अपान प्राणयो रैक्यं क्षयोमूल पुरीष्योः । युवाभवति वृद्धोऽपि सतनं मूलबन्धनात् ।। —हठयोग प्रदीपिका
निरन्तर मूलबन्ध का अभ्यास करने से प्राण और अपान के समन्वय से—अनावश्यक मल नष्ट होते हैं और वृद्धता भी यौवन में बदलती है।
विलं प्रविष्टेव ततो व्रह्नाह्यंतरं व्रजेत् । तस्मान्नित्यं मूलबंधः कर्तव्यो योगिभिः सदा । —हठयोग प्र.
मूलबन्ध से कुण्डलिनी का प्रवेश ब्रह्मनाड़ी—सुषुम्ना—में होता है। इसलिए योगीजन नित्य ही मूलबन्ध का अभ्यास करें।
सिद्वये सर्वं भूतानि विश्वाधिष्ठानमद्वयम् । यस्मिन सिद्धिं गताः निद्धास्तासिद्धासनमुच्यते ।। यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम् । मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योउसौ ब्रह्मवादिनाम् ।। —तेजबिन्दु.
जो सर्वलोकों का मूल है। जो चित्त निरोध का मूल है, सो यह आत्मा ही ब्रह्मवादियों को सदा सेवन करना चाहिए। यही मूलबन्ध है। अन्यजुदा संकोचन रूप मूलबन्ध जिज्ञासुओं के लिए सेव्य नहीं है।
विलं प्रविष्टे ततो ब्रह्मनाडयन्तरं व्रजेत् । तस्मा न्नित्यं मूलबंधः कर्तव्यो योगिभिः सदा ।। —हठयोग प्रदीपिका 3।69
फिर जिस प्रकार सर्पिणी बिल में प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उद्दीप्त कुण्डलिनी ब्रह्मनाड़ी में प्रविष्ट होती है। इसीलिए योगियों को सदा ही मूलबन्ध का अभ्यास करना चाहिये।
मूलबन्ध एवं शक्तिचालिनी मुद्रा को विशिष्ट प्राणायाम कहा जा सकता है। सामान्य प्राणायाम में नासिका से सांस खींचकर प्राण प्रवाह को नीचे मूलाधार तक ले जाने और फिर ऊपर की ओर उसे वापिस लेकर नासिका द्वार से निकालते हैं। यही प्राण संचरण की क्रिया जब अधोभाग के माध्यम से की जाती है तो मूलबन्ध कहलाती है। नासिका का तो स्वभाव सांसें लेते और छोड़ते रहना है। अतः उसके साथ प्राण संचार का क्रम सुविधापूर्वक चल पड़ता है। गुदा अथवा उपस्थ इन्द्रियों द्वारा वायु खींचने जैसी कोई क्रिया नहीं होती अतः उस क्षेत्र के स्नायु संस्थान पर खिंचाव पैदा करके सीधे ही प्राण संचार का अभ्यास करना पड़ता है। प्रारम्भ में थोड़ा अस्वाभाविक लगता है किन्तु क्रमशः अभ्यास में आ जाता है।
मूलबन्ध में सुखासन, (सामान्य पालथी मार कर बैठना) पद्मासन (पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठना) सिद्धासन (मल-मूत्र छिद्रों के मध्य भाग पर एड़ी का दबाव डालना) इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
मल-द्वार को धीरे-धीरे सिकोड़ा जाय और ऐसा प्रयत्न किया जाय कि उस मार्ग से वायु खींचने के लिए संकोचन क्रिया की जा रही है। मल का वेग अत्यधिक हो और तत्काल शौच जाने का अवसर न हो तो उसे रोकने के लिए मल मार्ग को सिकोड़ने और ऊपर खींचने जैसी चेष्टा करनी पड़ती है। ऐसा ही मूलबन्ध में भी किया जाता है। मल द्वार को ही नहीं उस सारे क्षेत्र को सिकोड़ने का ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि मानो वायु अथवा जल को उस छिद्र से खींच रहे हैं। वज्रोली क्रिया में मूत्र मार्ग से पिचकारी की तरह जल ऊपर खींचने और फिर निकाल देने का अभ्यास किया जाता है। मूलबन्ध में जल आदि खींचने की बात तो नहीं है, पर संकल्प बल से गुदा द्वार ही नहीं मूत्र छिद्र से भी वायु खींचने जैसा प्रयत्न किया जाता है और उस सारे क्षेत्र को ऊपर खींचने का प्रयास चलता है गुदा मार्ग से वायु खींचकर नाभि से ऊपर तक घसीट ले जाने की चेष्टा आरम्भिक है। कुछ अधिक समय तक रुकना संभव होता है तो अपान को नाभि से ऊपर हृदय तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। यह खींचने का ऊपर ले जाने का पूर्वार्ध हुआ।
उत्तरार्ध में प्राणवायु को नाभि से नीचे की ओर लाया जाता है और अपान अपनी जगह आ जाता है। इसका व्यावहारिक स्वरूप यह है कि खींचने सिकोड़ने की क्रिया को ढीला छोड़ने, नीचे उतारने, खाली करने का वैसा ही प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि प्राणायाम में रेचन के लिये सांस छोड़ी जाती है।
मोटेतौर से उसे गुदा मार्ग को, मूत्र मार्ग को ऊपर की ओर सिकोड़ने की—पूरा संकोचन हो जाने पर कुछ देर रोके रहने की अन्ततः उसे ढीला छोड़ देने की गुदा मार्ग से होने वाली प्राणायाम क्रिया कहा जा सकता है।
स्मरण रहे कि यह क्रिया वायु संचार की नहीं प्राण संचार की है। नासिका द्वारा तो वायु संचार क्रम चलता ही रहता है, अतः उसके साथ प्राण प्रक्रिया जोड़ने में कठिनाई नहीं होती। मूलाधार क्षेत्र में श्वास लेने जैसा अभ्यास किसी इन्द्रिय को नहीं है, किन्तु प्राण संचार की क्षमता उस क्षेत्र में ऊर्ध्वभाग से किसी भी प्रकार कम नहीं। मूलबन्ध द्वारा प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाना प्रथम चरण है। दूसरे चरण में शक्तिचालनी मुद्रा के अभ्यास से प्राण, अपान आदि शरीरस्थ प्राणों को इच्छानुसार समुचित अनुपात में एक-दूसरे से जोड़ा, मिलाया जाना सम्भव होता है। ऐसा करने से शरीरस्थ पंच प्राण महाप्राण से संबद्ध हो जाते हैं।
गीता में योग साधक द्वारा प्राण को अपान में तथा अपान को प्राण में होमने का उल्लेख इसी दृष्टि से किया गया है। यथा :—
अपाने जुह्वति प्राणः प्राणोऽपान तथा परे । प्राणवान गतिं रूद्ववा प्राणायाम परायणाः ।।
अर्थात्—कोई साधक अपान में प्राण को आहुति देते हैं, कुछ प्राण में अपान को होमते हैं। प्राण और अपान की गति नियन्त्रित करके साधक प्राणायाम परायण होता है। नासिका द्वारा प्राण संचार करके उसे मूलाधार तक ले जाना प्राण को अपान में होमना है, और मूलबन्ध एवं शक्तिचालिनी मुद्रा आदि द्वारा ‘अपान’ का उत्थान करके उसे प्राण से मिलाना—अपान को प्राण में होमना कहा जाता है। प्राण और अपान दोनों की ही सामान्य गति को नियन्त्रित करके उसे उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना ही प्राणायाम का उद्देश्य है।
शक्तिचालनी मुद्रा का महत्व एवं लाभ योग शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है—
शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समाचारेत् । आयुर्वृद्धिर्भवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम् ।। —शिवसंहिता
शक्तिशालिनी मुद्रा का प्रतिदिन जो अभ्यास करता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है।
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिता । सा शक्तिश्चालिता येन संयुक्तो नात्र सशयः ।। —हठयोग प्रदीपिका
कुण्डलिनी सर्पिणी की तरह कुटिल है, उसे शक्तिचालनी मुद्रा द्वारा जो चलायमान कर लेता है वही योगी है।
शक्तिचालन की महत्ता में जो कुछ कहा गया है वह अतिशयोक्ति नहीं। यह विज्ञान सम्मत है। शक्ति कहीं से आती नहीं, सुप्त से जागृत, जड़ से चलायमान हो जाना ही शक्ति का विकास कहा जाता है। बिजली के जनरेटर में बिजली कहीं से आती नहीं है। चुम्बकीय क्षेत्र में सुक्वायल घुमाने से उसके अन्दर के इलेक्ट्रॉन विशेष दिशा में चल पड़ते हैं। यह चलने की प्रवृत्ति विद्युत संवाहक शक्ति (ई.एम.एफ.) के रूप में देखी जाती है। शरीरस्थ विद्युत को भी इसी प्रकार दिशा विशेष में प्रवाहित किया जा सके तो शरीर संस्थान एक सशक्त जेनरेटर की तरह सक्षम एवं समर्थ बन सकता है। योग साधनायें इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।