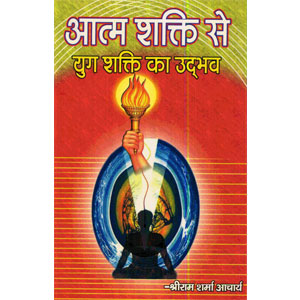आत्म-शक्ति से युग-शक्ति का उद्भव 
तन्मयता एवं नियमितता आवश्यक
Read Scan Version
उपासना में एकाग्रता पर बहुत जोर दिया गया है ध्यान धारणा का अभ्यास इसीलिए किया जाता है कि मन की अनियन्त्रित भगदड़ करने की आदत पर नियन्त्रण स्थापित किया जाये और उसे तथ्य विशेष पर केन्द्रित होने के लिए प्रशिक्षण किया जाय।
एकाग्रता एक उपयोगी सत्प्रवृत्ति है। मन की अनियन्त्रित कल्पनायें अनावश्यक उड़ानें उस उपयोगी विचार शक्ति का अपव्यय करती हैं जिसे यदि लक्ष्य विशेष पर केन्द्रित किया गया होता तो गहराई में उतरने और महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त करने का अवसर मिलता। यह चित्त की चंचलता ही है जो मनः संस्थान की दिव्य क्षमता को ऐसे ही निरर्थक गंवाती और नए भ्रष्ट करती रहती है। संसार के वे महामानव जिन्होंने किसी विषय में पारंगत प्रवीणता प्राप्त की है या महत्वपूर्ण सफलतायें उपलब्ध की हैं उन सबको विचारों पर नियन्त्रण करने—उन्हें अनावश्यक चिन्तन से हटा कर उपयोगी दिशा में चलाने की क्षमता प्राप्त रही है। इसके बिना चंचलता की वानर वृत्ति से ग्रसित व्यक्ति न किसी प्रसंग पर गहराई के साथ सोच सकता है और न किसी कार्यक्रम पर देर तक स्थिर रह सकता है। शिल्प, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण सभी प्रयोजनों की सफलता में एकाग्रता की शक्ति ही प्रधान भूमिका निभाती है। चंचलता को तो असफलता की सगी बहिन माना जाता है। बाल चपलता का मनोरंजक उपहास उड़ाया जाता है। वयस्क होने पर भी यदि कोई चंचल ही बना रहे विचारों की दिशाधारा बनाने और चिन्तन पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफल न हो सके तो समझना चाहिए कि आयु बढ़ जाने पर भी उसका मानसिक स्तर बालकों जैसा ही बना हुआ है। ऐसे लोगों का भविष्य उत्साहवर्धक नहीं।
आत्मिक प्रगति के लिए तो एकाग्रता की और भी अधिक उपयोगिता है। इसलिए ‘मेडीटेशन’ के नाम पर उसका अभ्यास विविध प्रयोगों द्वारा कराया जाता है। इस अभ्यास के लिए कोलाहल रहित ऐसे स्थान की आवश्यकता समझी जाती है जहां विक्षेपकारी आवागमन या कोलाहल न होता हो। एकान्त का तात्पर्य जनशून्य स्थान नहीं वरन् विक्षेप रहित वातावरण है। सामूहिकता हर क्षेत्र में उपयोगी मानी है। प्रार्थनायें सामूहिक ही होती हैं। उपासना भी सामूहिक हो तो उसमें हानि नहीं लाभ ही है। मस्जिदों में नमाज-गिरजा घरों में प्रेयर-मन्दिरों में आरती सामूहिक रूप से ही करने का रिवाज है। इसमें न तो एकान्त की कमी अखरती है और न एकाग्रता में कोई बाधा पड़ती है। एक दिशाधारा का चिन्तन हो रहा हो तो अनेक व्यक्तियों का समुदाय भी एक साथ मिल बैठकर एकाग्रता का अभ्यास भली प्रकार कर सकता है। एकान्त में बैठना वैज्ञानिक, तात्विक शोध अन्वेषण के लिए आवश्यक हो सकता है, उपासना के सामान्य सन्दर्भ में एकान्त ढूंढ़ने फिरने की ही कोई खास आवश्यकता नहीं है। सामूहिकता के वातावरण में ध्यान धारणा और भी अच्छी तरह बन पड़ती है। सेना का सामूहिक कार्य—साथ-साथ कदम मिलाकर चलने से—सैनिकों में से किसी का भी ध्यान नहीं बंटता वरन् साथ-साथ चलने की पग ध्वनि के प्रवाह में हर एक के पैर और भी अच्छी तरह अपने आप नियत क्रम से उठते चले जाते हैं। सहगमन से पग क्रम को ठीक रखने में बाधा नहीं पड़ती वरन् सहायता ही मिलती है। सहगान की तरह सहध्यान तथा सह भजन भी अधिक सफल और अधिक प्रखर बनता है।
उपासना के लिए जिस एकाग्रता का प्रतिपादन है उसका लक्ष्य है—भौतिक जगत की कल्पनाओं से मन को विरत करना और उसे अन्तर्जगत की क्रिया-प्रक्रिया में नियोजित कर देना। उपासना के समय यदि मन सांसारिक प्रयोजनों में न भटके और आत्मिक क्षेत्र की परिधि में परिभ्रमण करता रहे तो समझना चाहिए कि एकाग्रता का उद्देश्य ठीक तरह पूरा हो रहा है। विज्ञान के शोध कार्यों में—साहित्य के सृजन प्रयोजनों में वैज्ञानिक या लेखक का चिन्तन अपनी निर्धारित दिशा धारा में ही सीमित रहता है। इतने भर में एकाग्रता का प्रयोजन पूरा हो जाता है। यद्यपि इस प्रकार के बौद्धिक पुरुषार्थों में मन और बुद्धि को असाधारण रूप से गतिशील रहना पड़ता है और कल्पनाओं को अत्यधिक सक्रिय करना पड़ता है तो भी उसे चंचलता नहीं कहा जाता है। अपनी निर्धारित परिधि में रहकर कितना ही द्रुतगामी चिन्तन क्यों न किया जाय, कितनी ही कल्पनायें कितनी ही स्मृतियां, कितनी ही विवेचनायें क्यों न उभर रही हों वे एकाग्रता की स्थिति में तनिक भी विक्षेप उत्पन्न नहीं करेंगी। गड़बड़ तो अप्रासंगिकता में उत्पन्न होती है। बेतुका—बेसिलसिले का—अप्रासंगिक-अनावश्यक चिन्तन ही विक्षेप करता है। एक बेसुरा वादन पूरे आरकेस्ट्रा के ध्वनि प्रवाह को गड़बड़ा देता है, ठीक इसी प्रकार चिन्तन में अप्रासंगिक विक्षेपों का ही निषेध है। निर्धारित परिधि में कितनी ही कितने ही प्रकार की कल्पनायें-विवेचनायें करते रहने की पूरी पूरी छूट है।
कई व्यक्ति एकाग्रता का अर्थ मन की स्थिरता समझते हैं। और शिकायत करते हैं कि उपासना के समय उनका मन भजन में स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोग एकाग्रता और स्थिरता का अन्तर न समझने के कारण ही इस प्रकार की शिकायत करते हैं। मन की स्थिरता सर्वथा भिन्न बात है। उसे एकाग्रता से मिलती-जुलती स्थिति तो कहा जा सकता है पर दोनों का सीधा सम्बन्ध नहीं है। जिसका मन स्थिर हो उसे एकाग्रता का लाभ मिल सके या जिसे एकाग्रता की सिद्धि है उसे स्थिरता की प्राप्ति हो ही जाय यह आवश्यक नहीं है।
स्थिरता को निर्विकल्प समाधि कहा गया है और एकाग्रता को सविकल्प कहा गया है। सविकल्प का तात्पर्य है उस अवधि में आवश्यक विचारों का क्षेत्र में अपना काम करते रहना। निर्विकल्प का अर्थ है एक केन्द्र बिन्दु पर सारा चिन्तन सिमट कर स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाना।
यहां मनः संस्थान की संरचना को ध्यान में रखना होगा। मस्तिष्क की बनावट एक प्रचण्ड विद्युत भण्डार जैसी है। उसके भीतर और बाहरी क्षेत्र में विचार तरंगों के आंधी तूफान निरन्तर उठते रहते है। यह तरंग तूफान जितने तीव्र गति सम्पन्न होते हैं वह मस्तिष्क उतना ही उर्वरक और कुशाग्र बुद्धि माना जाता है। जहां इन तरंगों में जितनी मन्दगति हो समझना चाहिए कि वहां उतनी ही जड़ता, दीर्घसूत्रता, मूर्खता, छाई रहेगी। हारे थके मस्तिष्क को निद्रा घेर लेती है अर्थात उसकी गतिशीलता शिथिल हो जाती है। यह कृत्रिम निद्रा नशीली दवायें पिलाकर, क्लोरोफार्म, ईथर आदि सुंघाकर, सुन्न करने वाली दवा लगाकर उत्पन्न की जा सकती है। मूर्छा की स्थिति में मस्तिष्क की गतिशीलता ठप्प हो जाती है। स्थिरता ऐसे ही स्तर की हो सकती है। गड्ढ में बन्द होने के प्रदर्शन वाली जड़ समाधि में ऐसी ही स्थिरता होती है। मनस्वी लोग अपनी संकल्प शक्ति से हृदय की धड़कन और मस्तिष्क की सक्रियता को ठप्प कर देते हैं। स्थिरता जड़ समाधि के वर्ग में आती है। वह संकल्पशक्ति से या औषधियों से उत्पन्न की जा सकती है। स्थिरता का लाभ विश्राम मिलना है। इससे आन्तरिक थकान दूर हो सकती है और जिस तरह निद्रा के उपरान्त जागने पर नई चेतनता एवं स्फूर्ति का अनुभव होता है वैसा ही मन की स्थिरता का—निर्विकल्प समाधि का भी लाभ मिल सकता है। सामान्य रूप में इस स्थिति को शिथिलीकरण मुद्रा का एक प्रकार कहा जा सकता है। उसमें भी शरीर और मन की स्थिरता-शिथिलता-का ही अभ्यास किया जाता है। मैस्मरेजम-हिप्नोटिज्म प्रयोगों में भी इसी का अभ्यास काले गोल के माध्यम से करना पड़ता है। नेत्रों में वेधक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए एकाग्र मन-शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित करते है, मैस्मरेजम का यही आधार है। ऐसे ही सामान्य चमत्कार उस स्थिरता से उत्पन्न किये जा सकते हैं। जिसके लिए आमतौर से अध्यात्म साधना के विद्यार्थी लालायित रहते हैं और जिसके न मिलने पर अपने अभ्यास की असफलता अनुभव करके खिन्न होते हैं।
मन की स्थिरता अति कठिन है। वह हठयोग से ही सम्भव हो सकती है। तीन मिनट की स्थिरता मिल सके तो साधक शून्यावस्था में जाकर निद्रा ग्रस्त हो जाता है। जिन्हें निर्विकल्प समाधि अभीष्ट हो उन्हें ही स्थिरता की अपेक्षा और चेष्टा करनी चाहिए। जिन्हें सविकल्प साधना में स्थिरता को नहीं एक दिशाधारा में मन को नियोजित किये रहने की आवश्यकता है। पर ब्रह्म में आत्म समर्पण और उस परा-शक्ति का आत्म सत्ता में अवतरण ही ध्यान का मुख्य प्रयोजन है। उसके लिए कितने ही प्रकार की साकार-निराकार ध्यान धारणायें विद्यमान हैं, उनमें से जो उपयोगी एवं रुचिकर लगे उसे अपनाया जा सकता है।
स्थिरता स्तर की एकाग्रता हिप्नोटिज्म प्रयोगों में तो काम में आती ही है, सरकस के अनेक खेलों में भी मानसिक सन्तुलन ही चमत्कार दिखा रहा होता है। स्मरण शक्ति के धनी भी प्रायः एकाग्रता के ही अभ्यासी होते हैं। गणितज्ञों में तो यह विशेषता पाई ही जायगी। शोध कर्ताओं की सफलता का आधार यही है। उतने पर भी उसे आत्मिक प्रगति की अनिवार्य शर्त नहीं माना जा सकता। अधिक उसे सहायक ही कहा जा सकता है यदि ऐसा न होता तो यह सब एकाग्रता सम्पन्न लोग आत्मबल सम्पन्न हो गये होते और उनकी गणना सिद्ध योगियों में की जाने लगती। इसके विपरीत प्रायः सभी भावुक भक्त भावावेश जन्य चंचलता से ग्रस्त रहे हैं। मीरा, चैतन्य, रामतीर्थ रामकृष्ण परमहंस आदि इसी वर्ग के थे, जिन पर प्रायः भावावेश ही छाया रहता था। वे एकाग्र चित्त तो कदाचित् ही कभी हो पाते हों।
एकाग्रता के अभ्यास के लिए इष्ट देवताओं का निर्धारण करना होता है। उनकी चित्र, विचित्र आकृतियां, आभूषण, वस्त्र, आयुध, वाहन, इस दृष्टि से बनाये गये है कि ध्यान करने के लिए सुविस्तृत क्षेत्र मिल जाय। मन की दौड़ उन सब पर अदल-बदल—उछल-कूद करती रहती है। एक परिधि में मन को सीमित दौड़ लगाने का अवसर मिलता रहता है। पूर्ण एकाग्रता या स्थिरता की ध्यानयोग के आरम्भिक चरण में उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि समझी जाती है।
जिस एकाग्रता की आवश्यकता, अध्यात्म प्रगति के लिए बताई गई है वह मन की स्थिरता नहीं वरन् चिन्तन की दिशाधारा है। उपासना के समय सारा चिन्तन आत्मा का स्वरूप, क्षेत्र, लक्ष्य समझने में लगना चाहिए और यह प्रयास रहना चाहिए कि ब्राह्मी चेतना के गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर आत्मा की बहुमूल्य रत्नराशि संग्रह करने का अवसर मिले। उपासना का लक्ष्य स्थिर हो जाने पर उस समय जो विचार प्रवाह अपनाया जाना आवश्यक है उसे पकड़ सकना कुछ कठिन न रह जायगा।
मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का सार तत्व ‘तन्मयता’ शब्द में आ जाता है। गायत्री उपासना में यह प्रयोजन तन्मयता से पूरा होता है। तन्मयता का अर्थ है—इष्ट के साथ भाव संवेदनाओं को केन्द्रीभूत कर देना। यह स्थिति तभी आ सकती है जब इष्ट के प्रति असीम श्रद्धा हो। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब किसी की गरिमा पर परिपूर्ण विश्वास हो। साधक को अपनी मनोभूमि ऐसी बनानी चाहिए जिसमें गायत्री महाशक्ति की चरम उत्कृष्टता पर, असीम शक्ति सामर्थ्य पर, सम्पर्क में आने वाले के उत्कर्ष होने पर, गहरा विश्वास जमता चला जाये। यह कार्य शास्त्र वचनों का, अनुभवियों द्वारा बताये गये सत्परिणामों का, उपासना विज्ञान की प्रामाणिकता का, अधिकाधिक अध्ययन अवगाहन करने पर सम्पन्न होता है। आशंकाग्रस्त, अविश्वासी जन, उपेक्षा भाव से आधे अधूरे मन से उपासना में लगें तो स्वभावतः वहां उसकी रुचि नहीं होगी और मन जहां तहां उड़ता फिरेगा। मन लगने के लिए आवश्यक है कि उस कार्य में समुचित आकर्षण उत्पन्न किया जाय। व्यवसाय उपार्जन में इन्द्रिय भोगों में, विनोद मनोरंजनों में, सुखद कल्पनाओं में, प्रियजनों के सम्पर्क सान्निध्य में मन सहज ही लग जाता है। इसका कारण यह है कि इन प्रसंगों के द्वारा मिलने वाले सुख, लाभ एवं अनुभव के सम्बन्ध में पहले से ही विश्वास जमा होता है। प्रश्न यह नहीं कि वे आकर्षण दूरदर्शिता की दृष्टि से लाभदायक हैं या नहीं। तथ्य इतना ही है कि उन विषयों के सम्बन्ध में अनुभव अभ्यास के आधार पर मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया है। उस अकर्षण के फलस्वरूप ही मन उनमें रमता है और भाग-भागकर जहां-तहां घूम फिरकर वहीं जा पहुंचता है। हटाने से हटता नहीं, भगाने से भागता नहीं। मानसिक संरचना के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें उपासना के समय मन को इष्ट पर केन्द्रित रखने की आवश्यकता पूरी करने के लिए पहले से ही मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति के सन्दर्भ में जितना अधिक ज्ञान-विज्ञान संग्रह किया जा सके मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। विज्ञ व्यक्तियों के साथ उसकी चर्चा करनी चाहिए। इस सन्दर्भ में होने वाले सत्संगों में नियमित रूप से जाना चाहिए। जिसने लाभ उठाये हों उनके अनुभव सुनने चाहिए। यह कार्य यों तद् विषयक स्वाध्याय और मनन चिन्तन के एकाकी प्रयत्न से भी संभव हो सकता है, पर अधिक सरल और व्यवहारिक यह है कि गायत्री चर्चा के सन्दर्भ में चलने वाले सत्संगों में उत्साह पूर्वक नियमित रूप से सम्मिलित होते रहा जाय।
भूल यह होती रहती है कि किसी प्रकार जप संख्या पूरी कर लेने की ही उतावली रहती है और उसे ज्यों-त्यों पूरी कर लेना ही पर्याप्त मान लिया जाता है। यह स्मरण नहीं रखा जाता कि वाणी से मंत्रोच्चार करने, उंगलियों से माला फिराने के शारीरिक श्रम प्रयोजन से ही इतने महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती—उसके साथ मनोयोग और श्रद्धा का समावेश भी आवश्यक है। चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में तन्मयता सबसे बड़ा आधार है। शरीर से किये जाने वाले कर्मकाण्डों का प्रयोजन इतना ही है कि उनके कारण मस्तिष्क और अन्तःकरण को साथ-साथ चलने का आधार मिल जाय। चिन्तन का गहरा पुट रहने पर ही आत्मिक भूमिका में हलचलें होती हैं और प्रगति का सरंजाम जुटता है। यदि मन इष्ट पर जमे नहीं और मात्र उच्चारण का श्रम चलता रहे तो उसका भी लाभ तो मिलेगा पर इतना स्वल्प होगा जिससे अभीष्ट सत्परिणाम की अपेक्षा पूरी न हो सकेगी। अस्तु यह मानकर चलना चाहिए कि उपासना कृत्य में मनोयोग का लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।
तन्मयता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए धैर्य पूर्वक देर तक प्रयत्न करना होता है, यह एक दिन में सम्पन्न नहीं हो सकता। मन का पुराना अनुभव अभ्यास भौतिक आकर्षणों के साथ खेल करते रहने का है। उसे इससे विरत करने के लिए उससे अधिक नहीं कम से कम उतना बड़ा आकर्षण तो प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए। अरुचिकर प्रयोजन पर जमने की उसको आदत है ही नहीं। आकर्षण के अभाव में उसे बुरी तरह ऊब आती है और वहां से उचटने भागने की ऐसी धमाचौकड़ी मचाता है कि देर तक उस कार्य को चलाते रहना कठिन हो जाता है। तरह-तरह की बहानेबाजी बनाकर वहां से उठाने के लिए अचेतन मन कितनी-कितनी तरकीब खड़ी करता है यह सब देखते ही बनता है। खुजली उठना, जम्हाई आना, कोई साधारण सा खटका होते ही उधर देखने लगना, पालथी बदलना, कपड़े संभालना, जैसी चित्र-विचित्र क्रियाओं का होना यह प्रकट करता हैं कि मन यहां लग नहीं रहा और उस कार्य को छोड़कर जल्दी-जल्दी उठ चलने के लिए बार-बार तकाजा कर रहा है।
इस स्थिति का सामना करने के लिए प्रथम भूमिका यह है कि श्रद्धा जागृत करने वाले स्वाध्याय और सत्संग का—मनन और चिन्तन का ऐसा क्रम बनाया जाये जिससे उस दिशा में चलने के सत्परिणामों के सम्बन्ध में तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों के आधार उपासना के लिए श्रम करने की सार्थकता पर श्रद्धा और विश्वास गहरा होता चला जाय।
क्या सांसारिक क्या आध्यात्मिक सभी कार्यों में सुव्यवस्था, क्रमबद्धता, एवं नियमितता का भारी महत्व है अस्त-व्यस्त ढंग से अनियमित रीति से किये गये सभी काम काने-कुबड़े—आधे अधूरे और लंगड़े-लूले पड़े रहते हैं। जब कर्ता का क्रम ही व्यवस्थित नहीं तो किये गये काम में ही उत्कृष्टता कैसे दीख पड़ेगी। सफलता उन्हें मिलती है जो पहले अपनी गतिविधियों को सुव्यवस्थित बना लेते हैं। अस्त-व्यस्त रीति से काम करने वाले मनमानी बरतने वाले प्रायः हर काम में असफल रहते देखे जाते हैं। अनुशासन का सद्गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रगतिशीलता उसी के साथ जुड़ी हुई है।
आत्मिक प्रगति आत्मानुशासन से आरम्भ होती है। कई व्यक्ति उपासना के लिए बने हुए विधि-विधानों पर नियमोपनियमों पर ध्यान नहीं देते और मनमौजी स्वेच्छाचार बरतते हैं। ऐसा करने से उसके सत्परिणाम संदिग्ध रहते हैं। यह ठीक है कि प्राचीन काल की कई व्यवस्थायें इन दिनों असामयिक हो गई हैं और उनमें फेर बदल किये बिना कोई चारा नहीं। किन्तु वह परिवर्तन भी किसी सुनिश्चित आधार एवं सिद्धान्त के अनुरूप होना चाहिए। जिस परिवर्तन को मान्यता दे दी जाय फिर उसे तो उसी कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए जैसा कि परम्परावादियों का प्राचीन प्रचलनों पर जोर रहता है। यह अनुशासन एवं मर्यादा पालन ही आध्यात्म की भाषा में विश्वास कहा जाता है और उसका महत्व श्रद्धा के समतुल्य ही माना जाता है। कहा गया है कि श्रद्धा विश्वास के अभाव में धर्मानुष्ठान का महत्व उतना ही स्वल्प रह जाता है जितना कि काम में हलका-सा शारीरिक श्रम किया जाता है। शक्ति का स्रोत तो श्रद्धा एवं विश्वास ही हैं। इन्हीं दोनों को रामायणकार ने पार्वती और शिव की उपमा देते हुए कहा है कि इन दोनों के सहयोग से ही अन्तरात्मा में विराजमान परमेश्वर का दर्शन सम्भव हो सकता है।
श्रद्धा का सहचर है—विश्वास। इसे निष्ठा भी कहते हैं। किसी तथ्य को स्वीकार करने के पूर्व उस पर परिपूर्ण विचार कर लिया जाय। तर्क प्रमाण, परामर्श, परीक्षण आदि के आधार पर तथ्य का पता लगा लिया जाय और समुचित मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाय। इसमें देर लगे तो लगने देनी चाहिए। उतावली में इतना अधूरा निष्कर्ष न अपना लिया जाय जिससे किसी के तनिक से बहकावे मात्र से बदलने की बात सोची जाय। कई व्यक्ति विधि-विधानों के बारे में ऐसे ही अनिश्चित रहते हैं। एक के बाद दूसरे से पूछते फिरते हैं। फिर दूसरे का तीसरे और तीसरे का चौथे से समाधान पूछते हैं। भारतीय धर्म का दुर्भाग्य ही है कि इसमें पग-पग पर मतमेद के पहाड़ खड़े पाये जा सकते हैं। यदि मतभेद और शंकः-शंकाओं के जंजाल में उलझे रहा जाय तो उसका परिणाम मतिभ्रम-अश्रद्धा-अनिश्चितता एवं आशंका से मनःक्षेत्र भर जाने के अतिरिक्त और कुछ भी न होगा। ऐसी मनःस्थिति में किये गये धर्मानुष्ठानों का परिणाम नहीं के बराबर ही होता है। श्रद्धा-विश्वास का प्राण ही निकल गया तो फिर मात्र कर्मकाण्ड की लाश लादे फिरने से कोई प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा।
विश्वास का तात्पर्य है जिस तथ्य को मान्यता देना उस पर दृढ़ता के साथ आरूढ़ रहना। इस दृढ़ता का परिचय उपासनात्मक विधि-विधानों की जो मर्यादा निश्चित करली गई है उसे बिना आलस उपेक्षा बरते पूरी तत्परता के साथ अपनाये रहने में मिलता है। विधि-विधानों के पालन करने के लिए शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है और उसकी उपेक्षा करने पर साधन के निष्फल जाने अथवा हानि होने—निराशा हाथ लगने का—भय दिखाया गया है। उसका मूल उद्देश्य इतना ही है कि विधानों के पालन करने में दृढ़ता की नीति अपनाई जाय। हानि होने का भय दिखाने में इतना ही तथ्य है कि अभीष्ट सत्परिणाम नहीं मिलता। अन्यथा सत्प्रयोजन में कोई त्रुटि रह जाने पर भी अनर्थ की आशंका करने का तो कोई कारण है ही नहीं।
साधना मार्ग पर चलने वाले को अपनी स्थिति के अनुरूप विधि व्यवस्था का निर्धारण आरम्भ में ही कर लेना चाहिए। जो निश्चित हो जाय उसमें आलस उपेक्षा बरतने की ढील-पोल न दिखाई जाय। दृढ़ता न बरती जायगी तो आस्था में शिथिलता आने लगेगी। तत्परता मन्द पड़ जायगी फलतः मिलने वाला उत्साह और प्रकाश भी धूमिल हो जायगा।
उपासना के माध्यम से मनोनिग्रह के द्वारा एकाग्रता की शक्ति का उदय और ईश्वर सान्निध्य का लाभ मिलता है। आत्मिक प्रगति के लिए उन दोनों ही उपार्जनों की आवश्यकता है। मन ईश्वर के समीप बैठने के लिए सहमत हो इसके लिए उस सन्दर्भ में श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उपासना के सत्परिणामों पर जितना अधिक स्वाध्याय, सत्संग चिन्तन, मनन, अवगाहन किया जायगा उतनी ही श्रद्धा और अभिरुचि बढ़ेगी। इन उपचारों को भी जप ध्यान की ही तरह आवश्यक माना जाना चाहिए। यह योग पक्ष है।
उपासना का दूसरा पक्ष है तप। तप का अर्थ है—संयम, निग्रह, अनुशासन, प्रशिक्षण। उच्छृंखलता को निरस्त करके श्रेष्ठता की दिशा में मनोभूमि को बल पूर्वक घसीट ले चलने के लिए जो कड़ाई की जाती है उसी को, तपश्चर्या कहते हैं। बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए एक आंख प्यार की दूसरी सुधार की रखने की रीति अपनानी पड़ती है। मन को भी योग से प्यार और तप से सुधार की शिक्षा दी जाती है। दोनों ही अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों के ही समन्वय से दोनों पहिये सही होने पर ठीक तरह चलने वाली गाड़ी की तरह आत्मिक प्रगति की गतिशीलता सुव्यवस्थित, बनती, और सुचारु रूप से चलती रहती है।
आरम्भिक साधन को उपासना सम्बन्धी न्यूनतम नियमों का निर्धारण करना होता है। प्रतिदिन किस समय, कितनी देर तक साधना की जानी है, इसका निर्णय करना होता है। साथ ही यह निश्चय करना पड़ता है कि बिना अनिवार्य कारण आये उस समय की उपेक्षा न की जायेगी—उसमें आलस्य और प्रमाद को बाधक नहीं बनने दिया जायगा। ऐसे सुदृढ़ निश्चय को संकल्प कहते हैं। साधना की सफलता में संकल्प आवश्यक माना गया है। संकल्प प्रायः सभी धर्मानुयायियों में जुड़ा रहता है उसे विधान का आवश्यक अंग माना जाता है। संकल्प का अर्थ है जो निश्चय किया गया है उसे पूरा करने का मानसिक निश्चय एवं सम्बद्ध लोगों को उस निश्चय का परिचय। इस घोषणा का उद्देश्य है निर्धारित कार्य को पूरा करने की बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना। उसे पूरा न कर सकने पर अपनी अप्रतिष्ठा अनुभव करना।
आरम्भ भले ही न्यूनतम पन्द्रह मिनट का किया जाय पर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसके निर्वाह में किसी को भी बाधक नहीं होने दिया जायगा। वस्तुतः कोई और होता भी नहीं। मात्र मन की अरुचि ही सबसे बड़ी बाधा होती है। इसे दूर करने के लिए कठोरता का अंकुश लगाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। देखा गया है कि भावावेश में दस पांच दिन उपासना का आरम्भिक उत्साह चलता है और फिर तत्काल कोई बड़ा चमत्कार न मिलने से ऊब आने लगती है। उपेक्षा आरम्भ होती है, आलस्य चढ़ता है और किसी छोटे से बहाने की आड़ में वह क्रम समाप्त कर दिया जाता है। यह स्थिति हर साधक के सामने आती है। उसका सामना करने की मोर्चा बन्दी पहले से ही करली जानी चाहिए। संकल्प को हर हालत में पूरा करने का निश्चय करके चलना चाहिए। मन न लगने की कठिनाई आकर ही रहेगी, इस तथ्य को पहले से ही स्मरण रखना चाहिए।
नियत समय का पालन करने के लिए अलार्म घड़ी से सहायता ली जा सकती है। उसे मिलिट्री के बिगुल के समतुल्य माना जाय जिसके बजते ही सभी सैनिक तत्काल नियत स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। समय का पालन हर काम के लिए किया जाना चाहिए। प्रगतिशीलता का यह प्रमुख चिन्ह है। उसमें आलस्य को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। आलसी स्वभाव समय को जैसे तैसे गुजारने की बहानेबाजी करता रहता है। उसे न चलने देने में अपने शौर्य साहस का—उत्साह और संकल्प का परिचय देना चाहिए मन की विचित्रता एवं विशेषता यह है वह कुछ ही दिन के अभ्यास से भले या बुरे ढांचे में ढल जाता है। उसी का अभ्यस्त हो जाता है। नियत समय पर उपासना के लिए तैयार होने में आरम्भ के कुछ ही दिन अनभ्यस्त आलस के कारण बाधा पड़ेगी। यदि उसकी अवहेलना प्रताड़ना की जाती है और कड़ाई के साथ अनुशासन बरत कर उसे यथासमय, यथा स्थान बिठाया जा सके तो खींचतान बहुत दिन न चलेगी लगातार दबाव पड़ते रहने पर आदत उसी प्रकार की पड़ जायगी और फिर नियत समय पर न बैठना भी कष्ट कारक लगने लगेगा।
कभी-कभी कोई अनिवार्य कारण ऐसे भी आ सकते हैं जिनसे नियत समय पर बैठना सम्भव न हो सके। ऐसी दशा में यह व्रत पालन किया जाना चाहिए कि भोजन से अथवा सोने से पूर्व उस संकल्प साधना को अवश्य पूरा कर लिया जायगा। प्रातः छः बजे संकल्पित साधना न हो सकी तो दोपहर को भोजन के समय तक उसे पूरा कर लेना चाहिए। भोजन के लिए आखिर कभी तो समय निकलेगा ही। उसे पन्द्रह मिनट और भी पीछे खिसकाया जा सकता है। पूरे विधान से साधना न बन पड़े तो मानसिक जप के रूप में उसे पूरा किया जा सकता है। भोजन के समय भी न बन पड़े तो रात्रि को सोने से पूर्व उसे कर लेने के नियम में तो कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती। भोजन में अन्य लोगों के साथ रहने की अड़चन रह सकती है पर सोते समय तो वैसे भी कोई अड़चन नहीं होती। सोने का समय उतनी देर और खिसकाया जा सकता है जितनी देर कि नित्य नियम की उपासना पूरी करनी है। भोजन का विलम्ब या सोने का विलम्ब उतना नहीं अखरना चाहिए जितना कि उपासना क्रम का परित्याग। यदि संकल्प श्रद्धा युक्त हो—और उपासना को बेगार भुगतान न मानकर आत्मिक आवश्यकता माना गया हो तो उसे प्राथमिकता देने में तनिक भी असुविधा न होगी। उपेक्षा तो उसकी होती है जो निरर्थक माना जाय। भजन के सम्बन्ध में यदि अन्तः श्रद्धा जम नहीं सकी है और उसे लादी हुई बेगार माना गया है तो ही उपेक्षा करने के लिये जी होगा। जी की कच्चाई से ही समय टलता है और फुरसत न मिलने का उपहासास्पद बहाना बन कर खड़ा हो जाता है।
यदि कोई दिन सचमुच ही वैसा आ जाय जिसमें उपासना सम्भव न हो सके तो दूसरे दिन उसकी पूर्ति करने के लिए दूना समय लगाया जाना चाहिए। हो सके तो इसमें पांच मिनट प्रायश्चित्य ‘‘पैनलटी’’ ब्याज के रूप में और भी जोड़ देना चाहिए।
उपासना को अनिवार्य नित्य कर्म में सम्मिलित कर लेने और उसका कड़ाई के साथ निर्वाह कर लेने पर मन की आदत बदल जाती है। तब वह उचटना बन्द कर देता है और इसी में रस लेने लगता है। ध्यान लगा या नहीं यह प्रश्न बहुत पीछे का है। पहली बात तो इतनी ही है कि उसे आवश्यक कृत्य मानकर दिनचर्या में सम्मिलित किया गया या नहीं? मन की स्वीकृति इस प्रथम चरण में मिल सके तो समझना चाहिए कि उपासना में मन लगने की आधी समस्या हल हो गई।
मनोनिग्रह का प्रथम चरण इतना ही है कि वह उपासना के प्रति विद्रोह करना बन्द कर दे। नियत समय पर बैठने में अड़चन न उत्पन्न करे और जितनी देर भजन करना है उतना काल शान्ति पूर्वक व्यतीत हो जाने दे। ऊब उत्पन्न न करे। भाग चलने और छोड़ बैठने के लिए विद्रोह न करे। उसके विद्रोही स्वर शिथिल हो जायं। सहन करने और समन्वय बना लेने में बाधा न डाले तो समझना चाहिए आशाजनक स्थिति बन गई। भले ही वह इस बीच इधर उधर भटकता रहे और उपासना क्रम मन्त्रोच्चार एवं विधि विधान तक ही सीमित बना रहे तो भी काम चल जायगा। सहज, समन्वय की स्थिति यदि मन ने स्वीकार कर ली है तो फिर सहमति और सहयोग का सिलसिला चल पड़ने में भी देर न लगेगी।
मन के ऊपर कड़ाई से नियन्त्रण करने और अनुशासन स्थापित करने में संकल्प शक्ति जगाने की आवश्यकता पड़ती है। निश्चय और निर्धारण करना पड़ता है। घोषणा को पूरा करना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना पड़ता है। इसमें जितनी सफलता मिलती चलती है उतना ही संकल्प बल बढ़ता है। आत्मानुशासन रख सकने की क्षमता पर विश्वास होता है। छोटे-छोटे संकल्प करते चलना और उन्हें पूरा कर सकने की क्षमता का परिचय देना, यही है आत्म बल बढ़ाने का क्रमिक उपाय। आत्म विश्वास ही परिपक्व होकर आत्मबल बन जाता है। आत्मबल की महिमा धन, बल, बुद्धिबल, बाहुबल, कौशल बल, साधन बल आदि सभी से बढ़कर है। उसके सहारे भौतिक और आत्मिक सफलताओं के अवसर पग-पग पर मिलते चलते चले जाते हैं।
पानी को भाप बनाने में—दो लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ देने में गर्मी की ही भूमिका रहती है। सुस्वादु और सुपाच्य भोजन का निर्माण चूल्हे पर चढ़ाये जाने पर ही होता है। मशीनों के चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा अग्नि के सहारे ही उत्पन्न होती है। सूरज तपता है तो पृथ्वी गृह पर हलचलें होती हैं। शरीर में जब तक गर्मी है तभी तक जीवन है। अग्नि की—गर्मी की क्षमता सर्वत्र देखी जा सकती है। वस्तुतः गर्मी ही जीवन है। अण्डा हो अथवा भ्रूण उसे माता अपने शरीर की गर्मी देकर ही पकाती है। वनस्पतियों का उगना और फलना-फूलना गर्मी पर ही निर्भर है। ठण्डक की ऋतु में सब कुछ ठप्प हो जाता है। हरे-भरे पेड़ तक पत्ते गिरने से ठूंठ जैसे बन जाते हैं। सर्दी में दिन ही नहीं सिकुड़ता—हर प्रक्रिया पर शिथिलता छाई दीखती है।
भौतिक प्रगति में चेतना की गर्मी ही उत्पादन और विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। उत्साह, स्फूर्ति, साहस, उमंग, जीवट, श्रमशीलता जैसे गुणों में आन्तरिक उष्णता ही काम करती है। ओजस तेजस और वर्चस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में उभरने वाली ऊर्जा ही तो है। मनस्वी तेजस्वी और तपस्वी अपनी भीतरी प्रखरता का परिचय देते हैं। यह ऊष्मा जब कम पड़ती है तो मनुष्य आलसी, निराश, उदास, भयभीत बन जाता है। ऐसे ही साहस रहित व्यक्ति को कायर, क्लीव आदि शब्दों से तिरष्कृत किया जाता है। उन्हें पिछड़ेपन की दयनीय उपहासास्पद परिस्थितियों में दिन गुजारने पड़ते हैं।
प्रगति के लिए तपश्चर्या का पुरुषार्थ करना पड़ता है। भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में यह तथ्य एक जैसा काम करता है। और प्रगति में सफल हुए प्रत्येक व्यक्ति को अभीष्ट श्रम करना पड़ता है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, सैनिक, पहलवान, कलाकार, व्यवसायी, शिल्पी आदि सभी की सफलतायें उनके प्रयत्न, पुरुषार्थ, श्रम साहस पर निर्भर रहती हैं, इस प्रयत्न परायणता को एक प्रकार से भौतिक तपश्चर्या ही कहना चाहिए। जो इससे कतराते हैं वे दरिद्रता, दुर्बलता, अशिक्षा, उपेक्षा, शोषण आदि के शिकार होते और पग-पग पर आक्रमणों का अभावों का, असफलताओं का दुःख भोगते हैं।
आत्मिक जीवन में भी यही बात है। उस क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह तथ्य पर निर्भर है कि साधक में तपश्चर्या की साहसिकता किस मात्रा तक प्रचण्ड हो सकी। उपासना और साधना का तात्विक पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अध्यात्म विज्ञान का सारा ढांचा ही यह प्रेरणा देता है कि प्रगति के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न की जाय। ऊपर उठने के लिए, आगे उठने के लिए इस संसार में सर्वत्र ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वायुयान या राकेट आकाश में फेंकने हों अथवा क्रेन से वजन को ऊपर उठाना हो, हर हालत में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। पानी ऊपर से नीचे की ओर तो सहज ही गिर सकता है पर उसे कुंए से ऊपर खींचना हो तो साधन और सामर्थ्य दोनों को ही जुटाना पड़ता है। व्यक्तित्व को—अन्तःचेतना को ऊपर उठाने के लिए भी तपश्चर्या से उत्पन्न ऊर्जा के बिना काम नहीं चल सकता है। पैदल चलने को शरीर में शक्ति चाहिए। मोटर चलानी हो तो भी शक्ति की व्यवस्था जुटानी होती है। जीवन को ऊंचा उठाना हो, आगे बढ़ना हो तो समर्थता उत्पन्न करनी होगी।
सामर्थ्य आसमान से नहीं टपकती और न उधार—उपहार में किसी को मिलती है। उसे निजी प्रयत्न पुरुषार्थ से ही उपार्जित करना पड़ता है। देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने पर भी याचना मात्र से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। भिक्षुकों को भी उनकी प्रार्थना के आधार पर नहीं पात्रता के आधार पर ही अनुदान मिलते हैं। अपंगों को देखकर दया उपजती है, और उन्हें उदारता पूर्वक दिया जाता है। सत्कर्म परायण सन्तों को भी श्रद्धापूर्वक कुछ दिया जाता है। इसके विपरीत निकम्मे लोगों की याचना प्रायः ठुकरा ही दी जाती है। समर्थ भिखमंगों को जितना मिलता है इससे कहीं अधिक भत्सर्ना उन्हें सहनी पड़ती है। याचना किन शब्दों में कितनी देर की गई दानी उस पर ध्यान नहीं देते, देने की उमंग याचक की पात्रता पर ही निर्भर रहती है। देवताओं की यही परम्परा है। मनोकामनायें पूरी करने के लिए जिस-जिस आडम्बर के सहारे उन्हें फुसला लेना अति दुष्कर है। इस आधार पर आत्मिक प्रगति के सपने देखने वाले, देवताओं के आगे गिड़गिड़ाते रहने वाले प्रायः निराश असफल ही रहते देखे गये हैं।
आत्मिक प्रगति की दिशा में अभीष्ट सफलता प्राप्त करने वालों का इतिहास आदि से अन्त तक एक ही तथ्य प्रमाणित करता है कि उनने आवश्यक तपश्चर्या करके अपनी पात्रता विकसित की फलतः उन्हें विभूतियों, सिद्धियों से लाभान्वित होने का अवसर मिला। महामानवों से लेकर ऋषि महर्षियों तक की सफलतायें पूर्णतया उनकी तप साधना पर निर्भर रही है। मन्त्राराधन जादूगरी नहीं है। उसके पीछे प्रचण्ड तपश्चर्या की शक्ति ही चमत्कार प्रस्तुत करती है।
यथार्थता यह है कि भौतिक क्षेत्र की तरह ही आत्मिक क्षेत्र में भी आत्मपरिष्कार के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। उन्हीं के आधार पर वह क्षमता विकसित होती है जो अन्तर्जगत की प्रस्तुत दिव्य क्षमताओं को जगाकर किसी को विभूतिवान् बना सके। इसी आधार पर देवी अनुग्रह भी आकर्षित किये जाते हैं। वृक्षों का चुम्बकत्व बादलों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें पानी बरसाने के लिए विवश करता है। धातुओं की खदानें भी इसी आधार पर बनती और बढ़ती हैं कि जमा हुआ धातु भण्डार अपनी आकर्षण क्षमता से दूर-दूर तक फैले हुए सजातीय कणों को खींचता रहता है और उनके खिच-खिंचकर जमा होते रहने से खदान का आकार भण्डार बढ़ता रहता है। फूल खिलता है तो भौंरे प्रशंसा करने, मधुमक्खी याचना करने और तितली शोभा बढ़ाने के लिए अनायास ही जा पहुंचती हैं। अच्छे डिवीजन से पास छात्रों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश पाने तथा छात्रवृत्ति मिलने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। प्रतिभावानों को उनकी योग्यता के अनुरूप, पद, धन और मान अनायास ही मिलता जाता है। यही बात सिद्धान्ततः आत्मिक प्रगति की दिशा में अक्षरशः लागू होती है। साधक की पात्रता का विकास जिस अनुपात से होता है उसी क्रम में उसका वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। इन दिव्य उपलब्धियों का उद्गम अन्तः क्षेत्र में भी है और व्यापक ब्रह्म सत्ता से भी अजस्र अनुग्रह बरसते हैं। दोनों ही क्षेत्रों की उपलब्धियों से साधक निहाल होता है। इतने पर भी मूल तत्व जहां का तहां है। जो पाना है उसका मूल्य चुकाया जाना चाहिए। कुछ में तो इस संसार में कुछ भी मिलने का नियम नहीं है। जो पाया है जो पाना है उसका मूल्य पहले या पीछे चुकाने की बात को किसी भी प्रकार झुठलाया नहीं जा सकता।
मूल्य देकर खरीदने का सिद्धांत ही सही और सनातन है। घटिया चीजें स्वल्प मूल्य में और बढ़िया वस्तुएं महंगे दाम पर खरीदी जाती हैं। असली हीरा हजारों में और नकली थोड़े से पैसों में बिकता है। मूल्य के अनुरूप ही उनका महत्व और सम्मान है। जीवित दुधारू गाय बहुत दाम की आती है किन्तु मिट्टी की छोटी सी गाय कम पैसे में मिल सकती है। सस्ते और महंगे का अन्तर स्पष्ट है। जीवित गाय, दूध, बछड़ा, गोबर आदि बहुत कुछ देती है किन्तु खिलौना गाय से मात्र मनोरंजन ही हो सकता है। सस्ती पूजा पत्नी से जिन सिद्धियों की अपेक्षा की जाती है वे यदि किसी को मिल भी सकें तो नकली ही होंगी। उनसे तरह-तरह के ध्यान दृश्य देखने जैसे कौतुक कौतूहल मात्र ही सम्भव हो सकते हैं। उतने भर से आत्म कल्याण की अथवा दूसरों की सहायता कर सकने जैसी अध्यात्म क्षमता किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती।
भौतिक जगत में पुरुषार्थ और उसके प्रतिफल का—कर्म और भाग्य का सिद्धान्त पग-पग पर चरितार्थ होता है। पुरुषार्थी सफलता पाते और शेखचिल्ली कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ते रहते हैं। आत्मिक क्षेत्र का पुरुषार्थ तपश्चर्या है। याचना की तिरछी तरकीबें नहीं। यदि पुरुषार्थ की—पात्रता की—शर्त न रही होती तो हर याचना करने वाले की मनोकामनायें सहज ही पूरी होते रहने की परम्परा पाई जाती। तब किसी को पुरुषार्थ की कष्टसाध्य प्रक्रिया अपनाने की तनिक भी आवश्यकता न होती।
तथ्यों को समझा जा सके तो बहुमूल्य आत्मिक विभूतियों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुरुषार्थ करने का सिद्धान्त भी सहज ही समझ में आ जायगा। आत्मिक पुरुषार्थ का नाम तपश्चर्या है इसी मार्ग पर चलते हुए प्राचीनकाल के महान आत्मवेत्ता उच्चस्तरीय सफलता प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। भागीरथ का गंगावतरण—पार्वती का शिव वरण तप साधना से ही सम्भव हो सका था। तपस्वी दधीचि की अस्थियों से ही व्यापक असुर साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला वज्र बना। ध्रुव को परम पद तप से ही मिला। सप्त ऋषियों को उच्चस्तरीय गरिमा इसी आधार पर प्राप्त हुई। विश्वामित्र ने इसी शक्ति के आधार पर नई दुनिया बनाने का साहस किया था। परशुराम का तप ही उनके कुठार के रूप में संसार भर के अनाचार से लड़ सकने की क्षमता बनकर प्रकट हुआ था। शृंगी ऋषि के तप बल से ही उनकी मन्त्र शक्ति इतनी समर्थ हो सकी कि उनके आचार्यत्व में किया गया दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ सार्थक हो सका। मध्यकाल में भी भगवान बुद्ध से लेकर योगी अरविंद तक की परम्परा में तपश्चर्या ही प्रधान रही है।
असुर वर्ग की क्षमतायें भी तपश्चर्या के आधार पर ही उभरी थीं। पुराण साक्षी है कि हिरण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, मेघनाद, मारीच, वृत्तासुर, भस्मासुर, सहस्रबाहु असुरों ने प्रचण्ड सामर्थ्य तप के बल पर ही प्राप्त की थी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कितने ही नर-नारी तप साधना के सहारे उच्चस्तरीय आत्मशक्ति का सम्पादन कर सके हैं। गान्धारी ने नेत्र शक्ति, समय की दिव्य दृष्टि, कुन्ती की देव सन्तान, सुकन्या का पति की वृद्धता निवारण, सावित्री का यम संघर्ष, अनुसुइया द्वारा तीन देवों को बाल स्वरूप जैसे घटनाक्रमों में तप की क्षमता ही उभरती हुई दिखाई पड़ती है। लोक हित के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकने वाले महामानवों में विलक्षण क्षमता का विकास साधना शक्ति के सहारे ही हो सका था। चाणक्य, समर्थ रामदास, गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस आदि के द्वारा लोक हित के जो महत्वपूर्ण काम बन पड़े उसमें उनके तपस्वी जीवन की गरिमा प्रकट होती है। तप साधना के स्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकने पर उन सब में व्यक्तित्व को पवित्र परिष्कृत, प्रखर बनाने वाली कष्टसाध्य जीवनयापन प्रक्रिया का समावेश तो निश्चित रूप में ही रहेगा। सरलतापूर्वक, स्वल्प श्रम में पूजा-पाठ करके ईश्वर अनुग्रह और आत्मोत्कर्ष का लाभ किसी को भी नहीं मिल सका है। भगवत् भक्ति भावुकता मात्र नहीं है। जीवनयापन की रीति नीति में आदर्शवादिता के लिए कष्ट सहन करने की नीति का समावेश किए बिना उपासना का मूल प्रयोजन पूरा ही नहीं होता। जहां वास्तविकता न होगी वहां प्रखर प्रतिफल भी कहां से प्राप्त होगा। सम्पन्नता, विद्वता, बलिष्ठता, प्रतिभा कलाकारिता, जैसी भौतिक सम्पदायें प्राप्त करने के लिए जब पुरुषार्थ करना पड़ता है तो इन सबसे अत्यधिक मूल्यवान आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए तप साधना से बच कर कोई सस्ती सरल पगडण्डी कैसे निकल सकती है। आत्मिक प्रगति का राजमार्ग तपश्चर्या के बलबूते पर ही पार किया जाता है।
तप का तात्पर्य है गर्मी उत्पन्न करना। गर्मी रगड़ से उत्पन्न होती है। घर्षण ही ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। बिजली बनने से लेकर आग जलने तक समस्त प्रकार के ऊर्जा उत्पादनों का स्रोत घर्षण ही है। श्वास-प्रश्वास क्रिया की प्रतिक्रिया ही शरीर को जीवित रखने वाली गर्मी बनाये रहती है। तप का तात्पर्य है पशु प्रवृत्तियों के विरुद्ध दैवी प्रकृति का टकराव उत्पन्न कर देना। इसी संघर्ष से अध्यात्म क्षेत्र की वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे तप शक्ति के नाम से जाना जाता है। महान आध्यात्मिक प्रयोजन इसी शक्ति के सहारे सम्पन्न होते हैं। समुद्र मंथन से चौदह रत्न निकलने की कथा प्रसिद्ध है। जीवन मन्थन से भी इसी प्रकार का विभूति उत्पादन होता है।
पशु प्रवृत्तियों का निराकरण और उनके स्थान पर दैवी सत्प्रवृत्तियों का प्रतिष्ठान। यही है उपासना का—साधना का—योग साधना का—तपश्चर्या का एक मात्र उद्देश्य। आध्यात्मिक क्षेत्र की समस्त सफलतायें एक इसी केन्द्र पर केन्द्रीभूत हैं। सिद्धियों का उद्गम स्रोत यही है। इस क्षेत्र में जागृति एवं प्रगति उत्पन्न करने के लिए तपश्चर्या की जाती है।
नरक से निकाल कर स्वर्ग में पहुंचाने की क्षमता एकमात्र तपश्चर्या में ही है। इसलिए मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को तपस्वी बनाया था। विनोबा की माता भी अपने तीनों बालकों को ब्रह्मज्ञानी ब कर अपने परिवार को देवोपम सम्मान दिला गई। तप से स्वर्ग मिलता है। इस तथ्य के समर्थन में असंख्यों शास्त्र वचन और पौराणिक उपाख्यान उपलब्ध हैं। महामानवों की समूची बिरादरी वस्तुतः तपस्वियों की ही देव सेना है। उनमें से प्रत्येक ने अपनी पशु प्रवृत्तियों के साथ—दैवी आदर्शवादिता का संघर्ष कराया है। सामान्य लोगों पर स्वार्थांधता, भोग-लालसा और वासना-तृष्णा ही छाई रहती है जबकि महामानव दैवी परम्पराओं को इस प्रखरता के साथ अपनाते हैं कि उसके सम्मुख पशुता को परास्त होते और पलायन करते ही देखी जा सके। स्वार्थ-परमार्थ के संघर्ष में कौन विजयी होता है? पशु और देवता में से कौन जीतता है? उसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि मानवी आकांक्षा और श्रमशीलता अपना समर्थन और योगदान किस पक्ष को प्रदान करती है। इस संदर्भ में आन्तरिक महाभारत होना निश्चित है। उस धर्मयुद्ध में जिसको जितना शौर्य साहस एवं त्याग बलिदान प्रस्तुत करना पड़े। उसे उसी स्तर का तपस्वी कहा जा सकता है। जिसने जितनी शक्ति एकत्रित कर ली समझना चाहिए आत्मिक प्रगति का—अपूर्णता को पूर्णता में परिणत करने का लक्ष्य उसके उतना ही समीप आ गया। तप ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। उसी के आधार पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। उसी के सहारे शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। इसी क्षमता को जो जितना उत्पन्न-उपलब्ध करले समझना चाहिए कि उसकी आन्तरिक सम्पन्नता उसी स्तर तक समुन्नत हो गई।
आत्मिक प्रगति का जिनने महत्व समझा हो उन्हें उस उपलब्धि का उचित मूल्य चुकाने का भी साहस उत्पन्न करना चाहिए। सिद्धियां सदा ही पुरुषार्थियों को प्राप्त रही हैं। विजय श्री शूरवीरों के ही हिस्से में आई है। आध्यात्मिक क्षेत्र का शौर्य साहस—पौरुष पराक्रम तप साधना के रूप में ही जाना जाता है। यहां एक बात पूरी तरह स्मरण रखी जानी चाहिए कि अकारण काय कष्ट देने को नहीं—उच्चस्तरीय आदर्शों के परिपालन में शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना आवश्यक है इसी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तप साधन कहलाता है।
सुयोग्य, सफल और समर्थ लोगों के साथ मिल जुलकर रहने में बुद्धिमानी ही बुद्धिमानी है। चन्दन के समीप उगने वाले अन्य पौधे भी सुगन्धित हो जाते हैं। पारस और लोहे के स्पर्श से सोना बनने की बात प्रसिद्ध है। सत्संग की महिमा इतनी बढ़ी चढ़ी हो तो सघन समन्वय की महिमा उससे भी अधिक क्यों न होगी। ईश्वर निश्चित रूप में इस योग्य है कि उसके साथ बिना आगा पीछा सोचे जीवन व्यवसाय में साझेदारी की जा सकती है। इसमें ऐसा कोई जोखिम नहीं है जिसके लिए आरम्भ से असमंजस और अन्त में पश्चाताप करने की आवश्यकता पड़े।
भिक्षुक एकांगी होता है याचना से उसका स्तर गिरता है और तिरस्कार पूर्वक थोड़ा सा ही मिलता है। किन्तु मित्र, साथी, उत्तराधिकारी अथवा भागीदार की स्थिति दूसरी ही होती है। वह अधिकार और सम्मान पूर्वक अपने लिए उपयुक्त सुविधा प्राप्त कर लेता है। किन्तु स्मरण रहे साझेदारी के कुछ सिद्धान्त हैं। न्याय और नीति अपनाये रहने पर ही वह साझेदारी चलती है।
जीवन व्यवसाय में शरीर और आत्मा दोनों की ही साझेदारी है। इस कारखाने को चलने में दोनों की ही पूंजी और मेहनत लगती है। अस्तु आत्मा का भाग अधिक और शरीर का कम है। शरीर जड़ है। उसे मात्र औजार उपकरण, बाह्य सेवक की संज्ञा मिल सकती है। वह मशीन की तरह कार्य करता है। जीवन का सारा कारखाना आत्मा की चेतना और क्षमता पूंजी के सहारे चल रहा है। वह हाथ हटाले तो काया में तत्काल सड़न आरम्भ हो जायगी और जल्दी से जल्दी गाढ़ने, जलाने, बहाने आदि का प्रबन्ध करना होगा। व्यक्तित्व गरिमा काया पर नहीं चेतना के स्तर पर अवलम्बित है। अस्तु महत्व भी उसी का अधिक है। ऐसी दशा में उपार्जन के लाभ का बड़ा अंश भी उसी को मिलना चाहिए।
पर होता ठीक उल्टा है। शरीर सब कुछ हड़प जाता है और आत्मा की आवश्यकता पूर्णतया उपेक्षित ही बनी रहती है। उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। पेट और प्रजनन की दोनों ही आवश्यकताएं शरीर की हैं। वासना की तृप्ति इन्द्रियां चाहती हैं। मन मस्तिष्क की ग्यारहवी इन्द्रियां शरीर का एक अवयव हैं। इसकी भूख लोभ मोह की तृष्णा और अहंता की पूर्ति मांगती है। शरीर और मन की कितनी ही आवश्यकताएं परिवार से पूरी होती हैं। इसलिए वह परिवार भी शरीर के विस्तार क्षेत्र में ही सम्मिलित है।
असंख्य योनियों में परिभ्रमण करने के उपरान्त मनुष्य जन्म का सुर दुर्लभ अवसर मिलता है। इसका प्रयोजन एक ही है कि अपूर्णता को पूर्णता में परिणत किया जाय। भव बन्धनों से छुटकारा पाया जाय। अगली कक्षा देवत्व को उपलब्ध किया जाय। ईश्वरीय भंडार की सबसे बड़ी सम्पदा मानवी काया है। इससे बढ़कर और मूल्यवान पदार्थ परमात्मा के भंडार में है ही नहीं। जो अन्य प्राणियों को नहीं मिली उन विशेषताओं से सम्पन्न विभूतिवान शरीर मौज करने के लिए नहीं वरन् धरोहर के लिए इस निमित्त दिया है कि उससे विश्व उद्यान को अधिक समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान दिया जाय—हाथ बटाया जाय। इन प्रयोजनों की जितनी पूर्ति जीवन सम्पदा से हो सके समझना चाहिए आत्मा को उतना ही लाभांश मिला। जितना पेट प्रजनन के लिए लग गया उतना शरीर की भागीदारी में चला गया माना जाय। देखते हैं कि इस दृष्टि से आत्मा को घाटा ही घाटा है। शरीर की लिप्साएं पूरी करने के लिए अनेकों कुकृत्य तक करने पड़ते हैं। मरने पर शरीर तो श्मशान में समाप्त हो जाता है पर उन कुकर्मों का फल आत्मा को जन्म जन्मान्तरों तक दुर्गति सहने के रूप में भुगतना पड़ता है। बुद्धिमान बनने वाला मनुष्य जीवन के स्वरूप, मूल्य, उद्देश्य और उत्तरदायित्व को समझने में कितना मूर्ख सिद्ध होता है। इस विसंगति को देखते हुए भारी आश्चर्य होता है।
आत्म ज्ञान, आत्म बोध आत्म साक्षात्कार उस जागृति को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने स्वरूप और लक्ष्य को समझ सकने योग्य बन सके। जिस विवेक बुद्धि से आत्मा की स्थिति और प्रगति का निर्धारण कर सकना संभव होता है उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। मनुष्य जीवन के उपरान्त ईश्वर का दूसरा अनुग्रह यही है। किन्तु यह मिलता उसी को है जो आत्म कल्याण की महत्ता और आवश्यकता समझता है जिसे मोह मदिरा की खुमारी छाई हुई है उसके लिए न इस अनुकम्पा की आवश्यकता है और न उपयोगिता। ऐसे कुपात्रों को ऋतम्भरा प्रज्ञा का—गायत्री महा शक्ति का—अनुग्रह वरदान मिले भी तो कैसे? ब्रह्मविद्या का प्रत्येक सोपान अपने आपको जानने, आत्म कल्याण में लगने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है—शरीर का ही नहीं आत्मा का भी महत्व समझा जाय और सब कुछ शरीर पर ही निछावर न किया जाय कुछ तो आत्मा के लिए सोचा जाय।
प्रभु समर्पित जीवन से परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है समर्पण बड़ी बात है शरणागति में अपना कुछ बचता ही नहीं। सब कुछ उसका हो जाता है जिसको समर्पण किया है इसका स्वरूप समझना हो तो नाले का नदी में, ईंधन का आग में, पानी का दूध में, बूंद का समुद्र में, पतंगे का दीपक में, पति का पत्नी में विलय होते देखकर यह जानना चाहिए कि शरणागति की स्थिति में भक्त और भगवान का एकत्व अद्वैत किस स्तर का होता होगा। तब भक्त की अपनी कामना ही नहीं सत्ता भी समाप्त हो जाती है। और काया पर, मन पर, अन्तःकरण पर पूरी तरह इष्ट देव का ही अनुशासन छाया रहता है। इस स्थिति में पहुंचने पर भक्त भगवान एक हो जाते हैं दोनों की सत्ता में नाम मात्र का ही अन्तर रह जाता है।
समय श्रम की सम्पदा क्रिया रूप में और मन बुद्धि की विभूति चिंतन रूप में उपलब्ध है। इन दोनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाय तो शरीर की ही तरह आत्मा को भी अपनी आवश्यकतायें पूरी करने में इनका लाभ मिलता रहे। समय 24 घण्टे का होता है। इसमें सोने के लिए सात घण्टे आजीविका उपार्जन के लिए आठ घण्टे, अन्य कार्यों के लिए पांच घण्टे इस प्रकार बीस घण्टे शरीर यात्रा के लिए लगाये जा सकते हैं। इतने घण्टों को यदि आलस्य प्रमाद में न गंवा स्फूर्ति और उत्साह का समावेश करते हुए काम किया जाय तो सामान्य निर्वाह का शारीरिक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का क्रम बहुत ही शान्ति सरलता और सुव्यवस्था के साथ चलता रह सकता है। तृष्णा का तो कहीं अन्त नहीं लोभ और मोह की पूर्ति तो 24 घण्टे से भी अधिक बड़ा दिन होने लगे और दिन रात उपार्जन उपयोग में ही संलग्न रहा जाता रहे तो भी पूर्ति नहीं हो सकती। औसत भारतीय स्तर का जीवन क्रम सन्तोषजनक मान लिया जाय तो इतने समय में सब कुछ भली प्रकार पूरा होता रह सकता है। शेष चार घण्टे परमार्थ प्रयोजनों में भली प्रकार लगते रह सकते हैं। मन और बुद्धि का उपयोग सत्प्रयोजनों के लिए खाली घण्टों में होता रहने में तो कुछ कठिनाई है ही नहीं। सामान्य काम काज करते समय भी चिंतन की उत्कृष्टता की परिधि में नियोजित किया जा सकता है। कामुकता को—ईर्ष्या द्वेष की पाप और पतन की विचारणाओं एवं योजनाओं के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं लगाना पड़ता। सामान्य काम काज करते, फुरसत रहते सोते ऊंघते वह कल्पनायें मस्तिष्क में दौड़ती रहती हैं। और उन्हीं क्षणों में वह सब कुछ परिपक्व हो जाता है जो अवांछनीयता अपनाने के लिए आवश्यक है। अश्लील चिन्तन के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं निकालना पड़ता। ठीक इसी प्रकार परमार्थ प्रयोजन के लिए निर्धारित चार घण्टों के अतिरिक्त सामान्य काम काज के बीच भी मन बुद्धि से आत्मकल्याण की कल्पनायें करने और योजनाएं बनाने का पर्याप्त अवसर मिल सकता है।
तीसरी सम्पदा है धन इसके उपार्जन का भी शरीर और आत्मा के बीच न्यायोचित विभाजन होना चाहिए। जीवन में ईश्वर की हिस्सेदारी मानी जाय तो धन वैभव का एक अंश भी उसके निमित्त अर्पण किया जाना चाहिए, यह अंश कितना हो यह व्यक्ति की उदारता और परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। यह फैसला अपने अन्तःकरण को पंच मानकर निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह स्वतः ही करना चाहिए। यों होता तो यह रहा है कि सारी कमाई वासना तृष्णा और अहंता की वैश्याएं ही लुभा फुसला कर अपहरण करती रहीं हैं। आत्मा के पल्ले तो भूसी भी नहीं पड़ती है। उस पुराने अनियत अभ्यास को घटाने छोड़ने में हीला हुज्जत तो बहुत होगी। घर परिवार वालों से लेकर मित्र हितैषी स्वजन सम्बन्धी होने का दावा करने वालों तक की इस सम्बन्ध में एक स्वर से असहमति होगी कि ईश्वर के लिए आत्म कल्याण के लिए-परमार्थ के लिए भी कोई कहने लायक अंश निकाला जाये। वे नकली सुपाड़ी, नकली अगरबत्ती, अक्षत, रोली जैसे चार पैसों के अनुदान से अधिक कुछ त्याग करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता से लेकर सम्बद्ध स्वजनों तक का सारा परिवार इस बात का विरोधी होगा कि जीवन सम्पदा में से श्रम, समय, मन, बुद्धि अथवा धन का साधन का कोई महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजन के लिए लगाया जाय।
इस मोह परिवार का तो उल्टा दबाव यह रहता कि ईश्वर से किस बहाने अधिक भौतिक लाभ पाने का जुगाड़ बिठाया जाय। ऐसी दशा में ईश्वर के निमित्त साधनों की भागीदारी प्रस्तुत करने के लिए तथा कथित अपनों की सहमति प्राप्त कर सकना निश्चय ही टेढ़ी खीर है।
जो हो आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए हिमाच्छादित पर्वत शिखर पर चढ़ने जितना साहस जुटाया जाना आवश्यक है। इस साहसिकता का आरम्भिक परिचय जीवन में ईश्वर की साझेदारी स्वीकार करने और लाभांश को दोनों भागीदारों में वितरित करने का निश्चय अपनाकर ही दिया जा सकता है।
इस साझेदारी का स्मरण दिलाने और न्यायोचित विभाजन का तकाजा करने के लिए युग निर्माण योजना की सदस्यता की प्रारम्भिक शर्त में अंशदान को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। उसका न्यूनतम अंश एक घण्टा समय और दस पैसा नित्य ज्ञानघट के लिए लगाते रहने की बात कही गई है। ज्ञानघट इसी प्रयोजन के लिए स्थापित कराये गये हैं। इस दिशा में ध्यान देकर हम ईश्वर को साझेदारी का सिद्धान्त स्वीकार करते हैं। उस स्वीकृति के ऊपर मुहर लगाने हस्ताक्षर करने के रूप में ही यह न्यूनतम अंश है। यह आरम्भ है अन्त नहीं। यह बीजारोपण है वृक्ष नहीं। जिस प्रकार प्रयत्न करने पर हर व्यक्ति चार घण्टे रोज-समय का छटा भाग परमार्थ प्रयोजनों के लिए लगा सकता है उसी प्रकार यदि परमार्थ को नई सन्तान के रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो उसके लिए भी अर्थोपार्जन का अंश लगा सकना कुछ भी कठिन प्रतीत न होगा। प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि अंशदान की दृष्टि से पिछले दिनों से जो उदारता बरती जा रही है उसकी अपेक्षा इस बसन्त पर्व से उसका अनुपात बढ़ा ही दिया जाय। जबकि यहां यदाकदा तो कुछ होता रहता है पर नियमितता नहीं बरती जाती, उन्हें किसी न किसी रूप में इस क्रम को नियमित बनाने और दिनचर्या में सम्मिलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानघट की स्थापना में और ज्ञान यज्ञ के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुदान प्रस्तुत करते रहने में तो किसी को कृपणता बरतनी ही नहीं चाहिए।
ईश्वर से मांगने की बात उचित है पर साथ ही दूसरा पक्ष यह भी सोचना चाहिए कि उसकी पात्रता सिद्ध करने को अपनी ओर से उदारता अपनाने की शर्त पूरी की गई या नहीं। समर्पण के अनुपात से अनुग्रह मिलने का तथ्य यदि हृदयंगम किया जा सके तो हम यथार्थता के अधिक निकट होंगे। समर्थों की साझेदारी में लाभ ही लाभ है। विश्व माता वेद माता ईश्वरीय दिव्य सत्ता को यदि साहस पूर्वक अपने जीवन व्यवसाय में साझीदारी बनाया जा सके तो इसे असाधारण लाभ कमाने और बुद्धिमान सिद्ध होने के राजमार्ग पर चल पड़ना ही कहा जायगा। इस बार का बसन्त पर्व हममें से प्रत्येक को इसी स्तर की साहसिकता अपनाने की प्रेरणा लेकर आया है। उसे जो जितनी मात्रा में अपना सकेंगे वे उतने ही दूरदर्शी सिद्ध होंगे।
एकाग्रता एक उपयोगी सत्प्रवृत्ति है। मन की अनियन्त्रित कल्पनायें अनावश्यक उड़ानें उस उपयोगी विचार शक्ति का अपव्यय करती हैं जिसे यदि लक्ष्य विशेष पर केन्द्रित किया गया होता तो गहराई में उतरने और महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त करने का अवसर मिलता। यह चित्त की चंचलता ही है जो मनः संस्थान की दिव्य क्षमता को ऐसे ही निरर्थक गंवाती और नए भ्रष्ट करती रहती है। संसार के वे महामानव जिन्होंने किसी विषय में पारंगत प्रवीणता प्राप्त की है या महत्वपूर्ण सफलतायें उपलब्ध की हैं उन सबको विचारों पर नियन्त्रण करने—उन्हें अनावश्यक चिन्तन से हटा कर उपयोगी दिशा में चलाने की क्षमता प्राप्त रही है। इसके बिना चंचलता की वानर वृत्ति से ग्रसित व्यक्ति न किसी प्रसंग पर गहराई के साथ सोच सकता है और न किसी कार्यक्रम पर देर तक स्थिर रह सकता है। शिल्प, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण सभी प्रयोजनों की सफलता में एकाग्रता की शक्ति ही प्रधान भूमिका निभाती है। चंचलता को तो असफलता की सगी बहिन माना जाता है। बाल चपलता का मनोरंजक उपहास उड़ाया जाता है। वयस्क होने पर भी यदि कोई चंचल ही बना रहे विचारों की दिशाधारा बनाने और चिन्तन पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफल न हो सके तो समझना चाहिए कि आयु बढ़ जाने पर भी उसका मानसिक स्तर बालकों जैसा ही बना हुआ है। ऐसे लोगों का भविष्य उत्साहवर्धक नहीं।
आत्मिक प्रगति के लिए तो एकाग्रता की और भी अधिक उपयोगिता है। इसलिए ‘मेडीटेशन’ के नाम पर उसका अभ्यास विविध प्रयोगों द्वारा कराया जाता है। इस अभ्यास के लिए कोलाहल रहित ऐसे स्थान की आवश्यकता समझी जाती है जहां विक्षेपकारी आवागमन या कोलाहल न होता हो। एकान्त का तात्पर्य जनशून्य स्थान नहीं वरन् विक्षेप रहित वातावरण है। सामूहिकता हर क्षेत्र में उपयोगी मानी है। प्रार्थनायें सामूहिक ही होती हैं। उपासना भी सामूहिक हो तो उसमें हानि नहीं लाभ ही है। मस्जिदों में नमाज-गिरजा घरों में प्रेयर-मन्दिरों में आरती सामूहिक रूप से ही करने का रिवाज है। इसमें न तो एकान्त की कमी अखरती है और न एकाग्रता में कोई बाधा पड़ती है। एक दिशाधारा का चिन्तन हो रहा हो तो अनेक व्यक्तियों का समुदाय भी एक साथ मिल बैठकर एकाग्रता का अभ्यास भली प्रकार कर सकता है। एकान्त में बैठना वैज्ञानिक, तात्विक शोध अन्वेषण के लिए आवश्यक हो सकता है, उपासना के सामान्य सन्दर्भ में एकान्त ढूंढ़ने फिरने की ही कोई खास आवश्यकता नहीं है। सामूहिकता के वातावरण में ध्यान धारणा और भी अच्छी तरह बन पड़ती है। सेना का सामूहिक कार्य—साथ-साथ कदम मिलाकर चलने से—सैनिकों में से किसी का भी ध्यान नहीं बंटता वरन् साथ-साथ चलने की पग ध्वनि के प्रवाह में हर एक के पैर और भी अच्छी तरह अपने आप नियत क्रम से उठते चले जाते हैं। सहगमन से पग क्रम को ठीक रखने में बाधा नहीं पड़ती वरन् सहायता ही मिलती है। सहगान की तरह सहध्यान तथा सह भजन भी अधिक सफल और अधिक प्रखर बनता है।
उपासना के लिए जिस एकाग्रता का प्रतिपादन है उसका लक्ष्य है—भौतिक जगत की कल्पनाओं से मन को विरत करना और उसे अन्तर्जगत की क्रिया-प्रक्रिया में नियोजित कर देना। उपासना के समय यदि मन सांसारिक प्रयोजनों में न भटके और आत्मिक क्षेत्र की परिधि में परिभ्रमण करता रहे तो समझना चाहिए कि एकाग्रता का उद्देश्य ठीक तरह पूरा हो रहा है। विज्ञान के शोध कार्यों में—साहित्य के सृजन प्रयोजनों में वैज्ञानिक या लेखक का चिन्तन अपनी निर्धारित दिशा धारा में ही सीमित रहता है। इतने भर में एकाग्रता का प्रयोजन पूरा हो जाता है। यद्यपि इस प्रकार के बौद्धिक पुरुषार्थों में मन और बुद्धि को असाधारण रूप से गतिशील रहना पड़ता है और कल्पनाओं को अत्यधिक सक्रिय करना पड़ता है तो भी उसे चंचलता नहीं कहा जाता है। अपनी निर्धारित परिधि में रहकर कितना ही द्रुतगामी चिन्तन क्यों न किया जाय, कितनी ही कल्पनायें कितनी ही स्मृतियां, कितनी ही विवेचनायें क्यों न उभर रही हों वे एकाग्रता की स्थिति में तनिक भी विक्षेप उत्पन्न नहीं करेंगी। गड़बड़ तो अप्रासंगिकता में उत्पन्न होती है। बेतुका—बेसिलसिले का—अप्रासंगिक-अनावश्यक चिन्तन ही विक्षेप करता है। एक बेसुरा वादन पूरे आरकेस्ट्रा के ध्वनि प्रवाह को गड़बड़ा देता है, ठीक इसी प्रकार चिन्तन में अप्रासंगिक विक्षेपों का ही निषेध है। निर्धारित परिधि में कितनी ही कितने ही प्रकार की कल्पनायें-विवेचनायें करते रहने की पूरी पूरी छूट है।
कई व्यक्ति एकाग्रता का अर्थ मन की स्थिरता समझते हैं। और शिकायत करते हैं कि उपासना के समय उनका मन भजन में स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोग एकाग्रता और स्थिरता का अन्तर न समझने के कारण ही इस प्रकार की शिकायत करते हैं। मन की स्थिरता सर्वथा भिन्न बात है। उसे एकाग्रता से मिलती-जुलती स्थिति तो कहा जा सकता है पर दोनों का सीधा सम्बन्ध नहीं है। जिसका मन स्थिर हो उसे एकाग्रता का लाभ मिल सके या जिसे एकाग्रता की सिद्धि है उसे स्थिरता की प्राप्ति हो ही जाय यह आवश्यक नहीं है।
स्थिरता को निर्विकल्प समाधि कहा गया है और एकाग्रता को सविकल्प कहा गया है। सविकल्प का तात्पर्य है उस अवधि में आवश्यक विचारों का क्षेत्र में अपना काम करते रहना। निर्विकल्प का अर्थ है एक केन्द्र बिन्दु पर सारा चिन्तन सिमट कर स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाना।
यहां मनः संस्थान की संरचना को ध्यान में रखना होगा। मस्तिष्क की बनावट एक प्रचण्ड विद्युत भण्डार जैसी है। उसके भीतर और बाहरी क्षेत्र में विचार तरंगों के आंधी तूफान निरन्तर उठते रहते है। यह तरंग तूफान जितने तीव्र गति सम्पन्न होते हैं वह मस्तिष्क उतना ही उर्वरक और कुशाग्र बुद्धि माना जाता है। जहां इन तरंगों में जितनी मन्दगति हो समझना चाहिए कि वहां उतनी ही जड़ता, दीर्घसूत्रता, मूर्खता, छाई रहेगी। हारे थके मस्तिष्क को निद्रा घेर लेती है अर्थात उसकी गतिशीलता शिथिल हो जाती है। यह कृत्रिम निद्रा नशीली दवायें पिलाकर, क्लोरोफार्म, ईथर आदि सुंघाकर, सुन्न करने वाली दवा लगाकर उत्पन्न की जा सकती है। मूर्छा की स्थिति में मस्तिष्क की गतिशीलता ठप्प हो जाती है। स्थिरता ऐसे ही स्तर की हो सकती है। गड्ढ में बन्द होने के प्रदर्शन वाली जड़ समाधि में ऐसी ही स्थिरता होती है। मनस्वी लोग अपनी संकल्प शक्ति से हृदय की धड़कन और मस्तिष्क की सक्रियता को ठप्प कर देते हैं। स्थिरता जड़ समाधि के वर्ग में आती है। वह संकल्पशक्ति से या औषधियों से उत्पन्न की जा सकती है। स्थिरता का लाभ विश्राम मिलना है। इससे आन्तरिक थकान दूर हो सकती है और जिस तरह निद्रा के उपरान्त जागने पर नई चेतनता एवं स्फूर्ति का अनुभव होता है वैसा ही मन की स्थिरता का—निर्विकल्प समाधि का भी लाभ मिल सकता है। सामान्य रूप में इस स्थिति को शिथिलीकरण मुद्रा का एक प्रकार कहा जा सकता है। उसमें भी शरीर और मन की स्थिरता-शिथिलता-का ही अभ्यास किया जाता है। मैस्मरेजम-हिप्नोटिज्म प्रयोगों में भी इसी का अभ्यास काले गोल के माध्यम से करना पड़ता है। नेत्रों में वेधक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए एकाग्र मन-शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित करते है, मैस्मरेजम का यही आधार है। ऐसे ही सामान्य चमत्कार उस स्थिरता से उत्पन्न किये जा सकते हैं। जिसके लिए आमतौर से अध्यात्म साधना के विद्यार्थी लालायित रहते हैं और जिसके न मिलने पर अपने अभ्यास की असफलता अनुभव करके खिन्न होते हैं।
मन की स्थिरता अति कठिन है। वह हठयोग से ही सम्भव हो सकती है। तीन मिनट की स्थिरता मिल सके तो साधक शून्यावस्था में जाकर निद्रा ग्रस्त हो जाता है। जिन्हें निर्विकल्प समाधि अभीष्ट हो उन्हें ही स्थिरता की अपेक्षा और चेष्टा करनी चाहिए। जिन्हें सविकल्प साधना में स्थिरता को नहीं एक दिशाधारा में मन को नियोजित किये रहने की आवश्यकता है। पर ब्रह्म में आत्म समर्पण और उस परा-शक्ति का आत्म सत्ता में अवतरण ही ध्यान का मुख्य प्रयोजन है। उसके लिए कितने ही प्रकार की साकार-निराकार ध्यान धारणायें विद्यमान हैं, उनमें से जो उपयोगी एवं रुचिकर लगे उसे अपनाया जा सकता है।
स्थिरता स्तर की एकाग्रता हिप्नोटिज्म प्रयोगों में तो काम में आती ही है, सरकस के अनेक खेलों में भी मानसिक सन्तुलन ही चमत्कार दिखा रहा होता है। स्मरण शक्ति के धनी भी प्रायः एकाग्रता के ही अभ्यासी होते हैं। गणितज्ञों में तो यह विशेषता पाई ही जायगी। शोध कर्ताओं की सफलता का आधार यही है। उतने पर भी उसे आत्मिक प्रगति की अनिवार्य शर्त नहीं माना जा सकता। अधिक उसे सहायक ही कहा जा सकता है यदि ऐसा न होता तो यह सब एकाग्रता सम्पन्न लोग आत्मबल सम्पन्न हो गये होते और उनकी गणना सिद्ध योगियों में की जाने लगती। इसके विपरीत प्रायः सभी भावुक भक्त भावावेश जन्य चंचलता से ग्रस्त रहे हैं। मीरा, चैतन्य, रामतीर्थ रामकृष्ण परमहंस आदि इसी वर्ग के थे, जिन पर प्रायः भावावेश ही छाया रहता था। वे एकाग्र चित्त तो कदाचित् ही कभी हो पाते हों।
एकाग्रता के अभ्यास के लिए इष्ट देवताओं का निर्धारण करना होता है। उनकी चित्र, विचित्र आकृतियां, आभूषण, वस्त्र, आयुध, वाहन, इस दृष्टि से बनाये गये है कि ध्यान करने के लिए सुविस्तृत क्षेत्र मिल जाय। मन की दौड़ उन सब पर अदल-बदल—उछल-कूद करती रहती है। एक परिधि में मन को सीमित दौड़ लगाने का अवसर मिलता रहता है। पूर्ण एकाग्रता या स्थिरता की ध्यानयोग के आरम्भिक चरण में उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि समझी जाती है।
जिस एकाग्रता की आवश्यकता, अध्यात्म प्रगति के लिए बताई गई है वह मन की स्थिरता नहीं वरन् चिन्तन की दिशाधारा है। उपासना के समय सारा चिन्तन आत्मा का स्वरूप, क्षेत्र, लक्ष्य समझने में लगना चाहिए और यह प्रयास रहना चाहिए कि ब्राह्मी चेतना के गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर आत्मा की बहुमूल्य रत्नराशि संग्रह करने का अवसर मिले। उपासना का लक्ष्य स्थिर हो जाने पर उस समय जो विचार प्रवाह अपनाया जाना आवश्यक है उसे पकड़ सकना कुछ कठिन न रह जायगा।
मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का सार तत्व ‘तन्मयता’ शब्द में आ जाता है। गायत्री उपासना में यह प्रयोजन तन्मयता से पूरा होता है। तन्मयता का अर्थ है—इष्ट के साथ भाव संवेदनाओं को केन्द्रीभूत कर देना। यह स्थिति तभी आ सकती है जब इष्ट के प्रति असीम श्रद्धा हो। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब किसी की गरिमा पर परिपूर्ण विश्वास हो। साधक को अपनी मनोभूमि ऐसी बनानी चाहिए जिसमें गायत्री महाशक्ति की चरम उत्कृष्टता पर, असीम शक्ति सामर्थ्य पर, सम्पर्क में आने वाले के उत्कर्ष होने पर, गहरा विश्वास जमता चला जाये। यह कार्य शास्त्र वचनों का, अनुभवियों द्वारा बताये गये सत्परिणामों का, उपासना विज्ञान की प्रामाणिकता का, अधिकाधिक अध्ययन अवगाहन करने पर सम्पन्न होता है। आशंकाग्रस्त, अविश्वासी जन, उपेक्षा भाव से आधे अधूरे मन से उपासना में लगें तो स्वभावतः वहां उसकी रुचि नहीं होगी और मन जहां तहां उड़ता फिरेगा। मन लगने के लिए आवश्यक है कि उस कार्य में समुचित आकर्षण उत्पन्न किया जाय। व्यवसाय उपार्जन में इन्द्रिय भोगों में, विनोद मनोरंजनों में, सुखद कल्पनाओं में, प्रियजनों के सम्पर्क सान्निध्य में मन सहज ही लग जाता है। इसका कारण यह है कि इन प्रसंगों के द्वारा मिलने वाले सुख, लाभ एवं अनुभव के सम्बन्ध में पहले से ही विश्वास जमा होता है। प्रश्न यह नहीं कि वे आकर्षण दूरदर्शिता की दृष्टि से लाभदायक हैं या नहीं। तथ्य इतना ही है कि उन विषयों के सम्बन्ध में अनुभव अभ्यास के आधार पर मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया है। उस अकर्षण के फलस्वरूप ही मन उनमें रमता है और भाग-भागकर जहां-तहां घूम फिरकर वहीं जा पहुंचता है। हटाने से हटता नहीं, भगाने से भागता नहीं। मानसिक संरचना के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें उपासना के समय मन को इष्ट पर केन्द्रित रखने की आवश्यकता पूरी करने के लिए पहले से ही मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति के सन्दर्भ में जितना अधिक ज्ञान-विज्ञान संग्रह किया जा सके मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। विज्ञ व्यक्तियों के साथ उसकी चर्चा करनी चाहिए। इस सन्दर्भ में होने वाले सत्संगों में नियमित रूप से जाना चाहिए। जिसने लाभ उठाये हों उनके अनुभव सुनने चाहिए। यह कार्य यों तद् विषयक स्वाध्याय और मनन चिन्तन के एकाकी प्रयत्न से भी संभव हो सकता है, पर अधिक सरल और व्यवहारिक यह है कि गायत्री चर्चा के सन्दर्भ में चलने वाले सत्संगों में उत्साह पूर्वक नियमित रूप से सम्मिलित होते रहा जाय।
भूल यह होती रहती है कि किसी प्रकार जप संख्या पूरी कर लेने की ही उतावली रहती है और उसे ज्यों-त्यों पूरी कर लेना ही पर्याप्त मान लिया जाता है। यह स्मरण नहीं रखा जाता कि वाणी से मंत्रोच्चार करने, उंगलियों से माला फिराने के शारीरिक श्रम प्रयोजन से ही इतने महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती—उसके साथ मनोयोग और श्रद्धा का समावेश भी आवश्यक है। चेतना शक्ति के उत्थान परिष्कार में तन्मयता सबसे बड़ा आधार है। शरीर से किये जाने वाले कर्मकाण्डों का प्रयोजन इतना ही है कि उनके कारण मस्तिष्क और अन्तःकरण को साथ-साथ चलने का आधार मिल जाय। चिन्तन का गहरा पुट रहने पर ही आत्मिक भूमिका में हलचलें होती हैं और प्रगति का सरंजाम जुटता है। यदि मन इष्ट पर जमे नहीं और मात्र उच्चारण का श्रम चलता रहे तो उसका भी लाभ तो मिलेगा पर इतना स्वल्प होगा जिससे अभीष्ट सत्परिणाम की अपेक्षा पूरी न हो सकेगी। अस्तु यह मानकर चलना चाहिए कि उपासना कृत्य में मनोयोग का लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।
तन्मयता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए धैर्य पूर्वक देर तक प्रयत्न करना होता है, यह एक दिन में सम्पन्न नहीं हो सकता। मन का पुराना अनुभव अभ्यास भौतिक आकर्षणों के साथ खेल करते रहने का है। उसे इससे विरत करने के लिए उससे अधिक नहीं कम से कम उतना बड़ा आकर्षण तो प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए। अरुचिकर प्रयोजन पर जमने की उसको आदत है ही नहीं। आकर्षण के अभाव में उसे बुरी तरह ऊब आती है और वहां से उचटने भागने की ऐसी धमाचौकड़ी मचाता है कि देर तक उस कार्य को चलाते रहना कठिन हो जाता है। तरह-तरह की बहानेबाजी बनाकर वहां से उठाने के लिए अचेतन मन कितनी-कितनी तरकीब खड़ी करता है यह सब देखते ही बनता है। खुजली उठना, जम्हाई आना, कोई साधारण सा खटका होते ही उधर देखने लगना, पालथी बदलना, कपड़े संभालना, जैसी चित्र-विचित्र क्रियाओं का होना यह प्रकट करता हैं कि मन यहां लग नहीं रहा और उस कार्य को छोड़कर जल्दी-जल्दी उठ चलने के लिए बार-बार तकाजा कर रहा है।
इस स्थिति का सामना करने के लिए प्रथम भूमिका यह है कि श्रद्धा जागृत करने वाले स्वाध्याय और सत्संग का—मनन और चिन्तन का ऐसा क्रम बनाया जाये जिससे उस दिशा में चलने के सत्परिणामों के सम्बन्ध में तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों के आधार उपासना के लिए श्रम करने की सार्थकता पर श्रद्धा और विश्वास गहरा होता चला जाय।
क्या सांसारिक क्या आध्यात्मिक सभी कार्यों में सुव्यवस्था, क्रमबद्धता, एवं नियमितता का भारी महत्व है अस्त-व्यस्त ढंग से अनियमित रीति से किये गये सभी काम काने-कुबड़े—आधे अधूरे और लंगड़े-लूले पड़े रहते हैं। जब कर्ता का क्रम ही व्यवस्थित नहीं तो किये गये काम में ही उत्कृष्टता कैसे दीख पड़ेगी। सफलता उन्हें मिलती है जो पहले अपनी गतिविधियों को सुव्यवस्थित बना लेते हैं। अस्त-व्यस्त रीति से काम करने वाले मनमानी बरतने वाले प्रायः हर काम में असफल रहते देखे जाते हैं। अनुशासन का सद्गुण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रगतिशीलता उसी के साथ जुड़ी हुई है।
आत्मिक प्रगति आत्मानुशासन से आरम्भ होती है। कई व्यक्ति उपासना के लिए बने हुए विधि-विधानों पर नियमोपनियमों पर ध्यान नहीं देते और मनमौजी स्वेच्छाचार बरतते हैं। ऐसा करने से उसके सत्परिणाम संदिग्ध रहते हैं। यह ठीक है कि प्राचीन काल की कई व्यवस्थायें इन दिनों असामयिक हो गई हैं और उनमें फेर बदल किये बिना कोई चारा नहीं। किन्तु वह परिवर्तन भी किसी सुनिश्चित आधार एवं सिद्धान्त के अनुरूप होना चाहिए। जिस परिवर्तन को मान्यता दे दी जाय फिर उसे तो उसी कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए जैसा कि परम्परावादियों का प्राचीन प्रचलनों पर जोर रहता है। यह अनुशासन एवं मर्यादा पालन ही आध्यात्म की भाषा में विश्वास कहा जाता है और उसका महत्व श्रद्धा के समतुल्य ही माना जाता है। कहा गया है कि श्रद्धा विश्वास के अभाव में धर्मानुष्ठान का महत्व उतना ही स्वल्प रह जाता है जितना कि काम में हलका-सा शारीरिक श्रम किया जाता है। शक्ति का स्रोत तो श्रद्धा एवं विश्वास ही हैं। इन्हीं दोनों को रामायणकार ने पार्वती और शिव की उपमा देते हुए कहा है कि इन दोनों के सहयोग से ही अन्तरात्मा में विराजमान परमेश्वर का दर्शन सम्भव हो सकता है।
श्रद्धा का सहचर है—विश्वास। इसे निष्ठा भी कहते हैं। किसी तथ्य को स्वीकार करने के पूर्व उस पर परिपूर्ण विचार कर लिया जाय। तर्क प्रमाण, परामर्श, परीक्षण आदि के आधार पर तथ्य का पता लगा लिया जाय और समुचित मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाय। इसमें देर लगे तो लगने देनी चाहिए। उतावली में इतना अधूरा निष्कर्ष न अपना लिया जाय जिससे किसी के तनिक से बहकावे मात्र से बदलने की बात सोची जाय। कई व्यक्ति विधि-विधानों के बारे में ऐसे ही अनिश्चित रहते हैं। एक के बाद दूसरे से पूछते फिरते हैं। फिर दूसरे का तीसरे और तीसरे का चौथे से समाधान पूछते हैं। भारतीय धर्म का दुर्भाग्य ही है कि इसमें पग-पग पर मतमेद के पहाड़ खड़े पाये जा सकते हैं। यदि मतभेद और शंकः-शंकाओं के जंजाल में उलझे रहा जाय तो उसका परिणाम मतिभ्रम-अश्रद्धा-अनिश्चितता एवं आशंका से मनःक्षेत्र भर जाने के अतिरिक्त और कुछ भी न होगा। ऐसी मनःस्थिति में किये गये धर्मानुष्ठानों का परिणाम नहीं के बराबर ही होता है। श्रद्धा-विश्वास का प्राण ही निकल गया तो फिर मात्र कर्मकाण्ड की लाश लादे फिरने से कोई प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा।
विश्वास का तात्पर्य है जिस तथ्य को मान्यता देना उस पर दृढ़ता के साथ आरूढ़ रहना। इस दृढ़ता का परिचय उपासनात्मक विधि-विधानों की जो मर्यादा निश्चित करली गई है उसे बिना आलस उपेक्षा बरते पूरी तत्परता के साथ अपनाये रहने में मिलता है। विधि-विधानों के पालन करने के लिए शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है और उसकी उपेक्षा करने पर साधन के निष्फल जाने अथवा हानि होने—निराशा हाथ लगने का—भय दिखाया गया है। उसका मूल उद्देश्य इतना ही है कि विधानों के पालन करने में दृढ़ता की नीति अपनाई जाय। हानि होने का भय दिखाने में इतना ही तथ्य है कि अभीष्ट सत्परिणाम नहीं मिलता। अन्यथा सत्प्रयोजन में कोई त्रुटि रह जाने पर भी अनर्थ की आशंका करने का तो कोई कारण है ही नहीं।
साधना मार्ग पर चलने वाले को अपनी स्थिति के अनुरूप विधि व्यवस्था का निर्धारण आरम्भ में ही कर लेना चाहिए। जो निश्चित हो जाय उसमें आलस उपेक्षा बरतने की ढील-पोल न दिखाई जाय। दृढ़ता न बरती जायगी तो आस्था में शिथिलता आने लगेगी। तत्परता मन्द पड़ जायगी फलतः मिलने वाला उत्साह और प्रकाश भी धूमिल हो जायगा।
उपासना के माध्यम से मनोनिग्रह के द्वारा एकाग्रता की शक्ति का उदय और ईश्वर सान्निध्य का लाभ मिलता है। आत्मिक प्रगति के लिए उन दोनों ही उपार्जनों की आवश्यकता है। मन ईश्वर के समीप बैठने के लिए सहमत हो इसके लिए उस सन्दर्भ में श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उपासना के सत्परिणामों पर जितना अधिक स्वाध्याय, सत्संग चिन्तन, मनन, अवगाहन किया जायगा उतनी ही श्रद्धा और अभिरुचि बढ़ेगी। इन उपचारों को भी जप ध्यान की ही तरह आवश्यक माना जाना चाहिए। यह योग पक्ष है।
उपासना का दूसरा पक्ष है तप। तप का अर्थ है—संयम, निग्रह, अनुशासन, प्रशिक्षण। उच्छृंखलता को निरस्त करके श्रेष्ठता की दिशा में मनोभूमि को बल पूर्वक घसीट ले चलने के लिए जो कड़ाई की जाती है उसी को, तपश्चर्या कहते हैं। बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए एक आंख प्यार की दूसरी सुधार की रखने की रीति अपनानी पड़ती है। मन को भी योग से प्यार और तप से सुधार की शिक्षा दी जाती है। दोनों ही अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों के ही समन्वय से दोनों पहिये सही होने पर ठीक तरह चलने वाली गाड़ी की तरह आत्मिक प्रगति की गतिशीलता सुव्यवस्थित, बनती, और सुचारु रूप से चलती रहती है।
आरम्भिक साधन को उपासना सम्बन्धी न्यूनतम नियमों का निर्धारण करना होता है। प्रतिदिन किस समय, कितनी देर तक साधना की जानी है, इसका निर्णय करना होता है। साथ ही यह निश्चय करना पड़ता है कि बिना अनिवार्य कारण आये उस समय की उपेक्षा न की जायेगी—उसमें आलस्य और प्रमाद को बाधक नहीं बनने दिया जायगा। ऐसे सुदृढ़ निश्चय को संकल्प कहते हैं। साधना की सफलता में संकल्प आवश्यक माना गया है। संकल्प प्रायः सभी धर्मानुयायियों में जुड़ा रहता है उसे विधान का आवश्यक अंग माना जाता है। संकल्प का अर्थ है जो निश्चय किया गया है उसे पूरा करने का मानसिक निश्चय एवं सम्बद्ध लोगों को उस निश्चय का परिचय। इस घोषणा का उद्देश्य है निर्धारित कार्य को पूरा करने की बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना। उसे पूरा न कर सकने पर अपनी अप्रतिष्ठा अनुभव करना।
आरम्भ भले ही न्यूनतम पन्द्रह मिनट का किया जाय पर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसके निर्वाह में किसी को भी बाधक नहीं होने दिया जायगा। वस्तुतः कोई और होता भी नहीं। मात्र मन की अरुचि ही सबसे बड़ी बाधा होती है। इसे दूर करने के लिए कठोरता का अंकुश लगाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। देखा गया है कि भावावेश में दस पांच दिन उपासना का आरम्भिक उत्साह चलता है और फिर तत्काल कोई बड़ा चमत्कार न मिलने से ऊब आने लगती है। उपेक्षा आरम्भ होती है, आलस्य चढ़ता है और किसी छोटे से बहाने की आड़ में वह क्रम समाप्त कर दिया जाता है। यह स्थिति हर साधक के सामने आती है। उसका सामना करने की मोर्चा बन्दी पहले से ही करली जानी चाहिए। संकल्प को हर हालत में पूरा करने का निश्चय करके चलना चाहिए। मन न लगने की कठिनाई आकर ही रहेगी, इस तथ्य को पहले से ही स्मरण रखना चाहिए।
नियत समय का पालन करने के लिए अलार्म घड़ी से सहायता ली जा सकती है। उसे मिलिट्री के बिगुल के समतुल्य माना जाय जिसके बजते ही सभी सैनिक तत्काल नियत स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। समय का पालन हर काम के लिए किया जाना चाहिए। प्रगतिशीलता का यह प्रमुख चिन्ह है। उसमें आलस्य को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। आलसी स्वभाव समय को जैसे तैसे गुजारने की बहानेबाजी करता रहता है। उसे न चलने देने में अपने शौर्य साहस का—उत्साह और संकल्प का परिचय देना चाहिए मन की विचित्रता एवं विशेषता यह है वह कुछ ही दिन के अभ्यास से भले या बुरे ढांचे में ढल जाता है। उसी का अभ्यस्त हो जाता है। नियत समय पर उपासना के लिए तैयार होने में आरम्भ के कुछ ही दिन अनभ्यस्त आलस के कारण बाधा पड़ेगी। यदि उसकी अवहेलना प्रताड़ना की जाती है और कड़ाई के साथ अनुशासन बरत कर उसे यथासमय, यथा स्थान बिठाया जा सके तो खींचतान बहुत दिन न चलेगी लगातार दबाव पड़ते रहने पर आदत उसी प्रकार की पड़ जायगी और फिर नियत समय पर न बैठना भी कष्ट कारक लगने लगेगा।
कभी-कभी कोई अनिवार्य कारण ऐसे भी आ सकते हैं जिनसे नियत समय पर बैठना सम्भव न हो सके। ऐसी दशा में यह व्रत पालन किया जाना चाहिए कि भोजन से अथवा सोने से पूर्व उस संकल्प साधना को अवश्य पूरा कर लिया जायगा। प्रातः छः बजे संकल्पित साधना न हो सकी तो दोपहर को भोजन के समय तक उसे पूरा कर लेना चाहिए। भोजन के लिए आखिर कभी तो समय निकलेगा ही। उसे पन्द्रह मिनट और भी पीछे खिसकाया जा सकता है। पूरे विधान से साधना न बन पड़े तो मानसिक जप के रूप में उसे पूरा किया जा सकता है। भोजन के समय भी न बन पड़े तो रात्रि को सोने से पूर्व उसे कर लेने के नियम में तो कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती। भोजन में अन्य लोगों के साथ रहने की अड़चन रह सकती है पर सोते समय तो वैसे भी कोई अड़चन नहीं होती। सोने का समय उतनी देर और खिसकाया जा सकता है जितनी देर कि नित्य नियम की उपासना पूरी करनी है। भोजन का विलम्ब या सोने का विलम्ब उतना नहीं अखरना चाहिए जितना कि उपासना क्रम का परित्याग। यदि संकल्प श्रद्धा युक्त हो—और उपासना को बेगार भुगतान न मानकर आत्मिक आवश्यकता माना गया हो तो उसे प्राथमिकता देने में तनिक भी असुविधा न होगी। उपेक्षा तो उसकी होती है जो निरर्थक माना जाय। भजन के सम्बन्ध में यदि अन्तः श्रद्धा जम नहीं सकी है और उसे लादी हुई बेगार माना गया है तो ही उपेक्षा करने के लिये जी होगा। जी की कच्चाई से ही समय टलता है और फुरसत न मिलने का उपहासास्पद बहाना बन कर खड़ा हो जाता है।
यदि कोई दिन सचमुच ही वैसा आ जाय जिसमें उपासना सम्भव न हो सके तो दूसरे दिन उसकी पूर्ति करने के लिए दूना समय लगाया जाना चाहिए। हो सके तो इसमें पांच मिनट प्रायश्चित्य ‘‘पैनलटी’’ ब्याज के रूप में और भी जोड़ देना चाहिए।
उपासना को अनिवार्य नित्य कर्म में सम्मिलित कर लेने और उसका कड़ाई के साथ निर्वाह कर लेने पर मन की आदत बदल जाती है। तब वह उचटना बन्द कर देता है और इसी में रस लेने लगता है। ध्यान लगा या नहीं यह प्रश्न बहुत पीछे का है। पहली बात तो इतनी ही है कि उसे आवश्यक कृत्य मानकर दिनचर्या में सम्मिलित किया गया या नहीं? मन की स्वीकृति इस प्रथम चरण में मिल सके तो समझना चाहिए कि उपासना में मन लगने की आधी समस्या हल हो गई।
मनोनिग्रह का प्रथम चरण इतना ही है कि वह उपासना के प्रति विद्रोह करना बन्द कर दे। नियत समय पर बैठने में अड़चन न उत्पन्न करे और जितनी देर भजन करना है उतना काल शान्ति पूर्वक व्यतीत हो जाने दे। ऊब उत्पन्न न करे। भाग चलने और छोड़ बैठने के लिए विद्रोह न करे। उसके विद्रोही स्वर शिथिल हो जायं। सहन करने और समन्वय बना लेने में बाधा न डाले तो समझना चाहिए आशाजनक स्थिति बन गई। भले ही वह इस बीच इधर उधर भटकता रहे और उपासना क्रम मन्त्रोच्चार एवं विधि विधान तक ही सीमित बना रहे तो भी काम चल जायगा। सहज, समन्वय की स्थिति यदि मन ने स्वीकार कर ली है तो फिर सहमति और सहयोग का सिलसिला चल पड़ने में भी देर न लगेगी।
मन के ऊपर कड़ाई से नियन्त्रण करने और अनुशासन स्थापित करने में संकल्प शक्ति जगाने की आवश्यकता पड़ती है। निश्चय और निर्धारण करना पड़ता है। घोषणा को पूरा करना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना पड़ता है। इसमें जितनी सफलता मिलती चलती है उतना ही संकल्प बल बढ़ता है। आत्मानुशासन रख सकने की क्षमता पर विश्वास होता है। छोटे-छोटे संकल्प करते चलना और उन्हें पूरा कर सकने की क्षमता का परिचय देना, यही है आत्म बल बढ़ाने का क्रमिक उपाय। आत्म विश्वास ही परिपक्व होकर आत्मबल बन जाता है। आत्मबल की महिमा धन, बल, बुद्धिबल, बाहुबल, कौशल बल, साधन बल आदि सभी से बढ़कर है। उसके सहारे भौतिक और आत्मिक सफलताओं के अवसर पग-पग पर मिलते चलते चले जाते हैं।
तपनिष्ठा और योग बुद्धि जगायें—
गर्मी से दृढ़ता आती है यह तथ्य सर्व विदित है। कच्ची मिट्टी मुलायम होती है किन्तु उसके बने बर्तन आवे में पका दिये जायं वे धातु निर्मित पात्रों का काम देने लगते हैं। कच्ची ईंटों के बने मकान आये दिन टूटते-फूटते रहते हैं किन्तु भट्टे में पकी ईंटें पत्थर जैसी मजबूत हो जाती हैं। खदान से निकलते समय धातुयें मिट्टी मिली होती हैं। आग में पकाने के बाद वे शुद्ध होती हैं और असली रूप में प्रकट होती हैं। लोहे को फौलाद स्टेनलैस स्टील लौहभस्म आदि बनाने के लिए बार-बार तपाना ही एक मात्र उपाय है। आभूषण औजार आदि के रूप में परिणित होने के लिए धातुओं को गलाने जितने स्तर का तापमान सहना पड़ता है। सोने को खरा घोषित करने के लिए तपाया जाना ही प्रमुख कसौटी है।पानी को भाप बनाने में—दो लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ देने में गर्मी की ही भूमिका रहती है। सुस्वादु और सुपाच्य भोजन का निर्माण चूल्हे पर चढ़ाये जाने पर ही होता है। मशीनों के चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा अग्नि के सहारे ही उत्पन्न होती है। सूरज तपता है तो पृथ्वी गृह पर हलचलें होती हैं। शरीर में जब तक गर्मी है तभी तक जीवन है। अग्नि की—गर्मी की क्षमता सर्वत्र देखी जा सकती है। वस्तुतः गर्मी ही जीवन है। अण्डा हो अथवा भ्रूण उसे माता अपने शरीर की गर्मी देकर ही पकाती है। वनस्पतियों का उगना और फलना-फूलना गर्मी पर ही निर्भर है। ठण्डक की ऋतु में सब कुछ ठप्प हो जाता है। हरे-भरे पेड़ तक पत्ते गिरने से ठूंठ जैसे बन जाते हैं। सर्दी में दिन ही नहीं सिकुड़ता—हर प्रक्रिया पर शिथिलता छाई दीखती है।
भौतिक प्रगति में चेतना की गर्मी ही उत्पादन और विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। उत्साह, स्फूर्ति, साहस, उमंग, जीवट, श्रमशीलता जैसे गुणों में आन्तरिक उष्णता ही काम करती है। ओजस तेजस और वर्चस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में उभरने वाली ऊर्जा ही तो है। मनस्वी तेजस्वी और तपस्वी अपनी भीतरी प्रखरता का परिचय देते हैं। यह ऊष्मा जब कम पड़ती है तो मनुष्य आलसी, निराश, उदास, भयभीत बन जाता है। ऐसे ही साहस रहित व्यक्ति को कायर, क्लीव आदि शब्दों से तिरष्कृत किया जाता है। उन्हें पिछड़ेपन की दयनीय उपहासास्पद परिस्थितियों में दिन गुजारने पड़ते हैं।
प्रगति के लिए तपश्चर्या का पुरुषार्थ करना पड़ता है। भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में यह तथ्य एक जैसा काम करता है। और प्रगति में सफल हुए प्रत्येक व्यक्ति को अभीष्ट श्रम करना पड़ता है। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, सैनिक, पहलवान, कलाकार, व्यवसायी, शिल्पी आदि सभी की सफलतायें उनके प्रयत्न, पुरुषार्थ, श्रम साहस पर निर्भर रहती हैं, इस प्रयत्न परायणता को एक प्रकार से भौतिक तपश्चर्या ही कहना चाहिए। जो इससे कतराते हैं वे दरिद्रता, दुर्बलता, अशिक्षा, उपेक्षा, शोषण आदि के शिकार होते और पग-पग पर आक्रमणों का अभावों का, असफलताओं का दुःख भोगते हैं।
आत्मिक जीवन में भी यही बात है। उस क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह तथ्य पर निर्भर है कि साधक में तपश्चर्या की साहसिकता किस मात्रा तक प्रचण्ड हो सकी। उपासना और साधना का तात्विक पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अध्यात्म विज्ञान का सारा ढांचा ही यह प्रेरणा देता है कि प्रगति के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न की जाय। ऊपर उठने के लिए, आगे उठने के लिए इस संसार में सर्वत्र ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वायुयान या राकेट आकाश में फेंकने हों अथवा क्रेन से वजन को ऊपर उठाना हो, हर हालत में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। पानी ऊपर से नीचे की ओर तो सहज ही गिर सकता है पर उसे कुंए से ऊपर खींचना हो तो साधन और सामर्थ्य दोनों को ही जुटाना पड़ता है। व्यक्तित्व को—अन्तःचेतना को ऊपर उठाने के लिए भी तपश्चर्या से उत्पन्न ऊर्जा के बिना काम नहीं चल सकता है। पैदल चलने को शरीर में शक्ति चाहिए। मोटर चलानी हो तो भी शक्ति की व्यवस्था जुटानी होती है। जीवन को ऊंचा उठाना हो, आगे बढ़ना हो तो समर्थता उत्पन्न करनी होगी।
सामर्थ्य आसमान से नहीं टपकती और न उधार—उपहार में किसी को मिलती है। उसे निजी प्रयत्न पुरुषार्थ से ही उपार्जित करना पड़ता है। देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने पर भी याचना मात्र से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। भिक्षुकों को भी उनकी प्रार्थना के आधार पर नहीं पात्रता के आधार पर ही अनुदान मिलते हैं। अपंगों को देखकर दया उपजती है, और उन्हें उदारता पूर्वक दिया जाता है। सत्कर्म परायण सन्तों को भी श्रद्धापूर्वक कुछ दिया जाता है। इसके विपरीत निकम्मे लोगों की याचना प्रायः ठुकरा ही दी जाती है। समर्थ भिखमंगों को जितना मिलता है इससे कहीं अधिक भत्सर्ना उन्हें सहनी पड़ती है। याचना किन शब्दों में कितनी देर की गई दानी उस पर ध्यान नहीं देते, देने की उमंग याचक की पात्रता पर ही निर्भर रहती है। देवताओं की यही परम्परा है। मनोकामनायें पूरी करने के लिए जिस-जिस आडम्बर के सहारे उन्हें फुसला लेना अति दुष्कर है। इस आधार पर आत्मिक प्रगति के सपने देखने वाले, देवताओं के आगे गिड़गिड़ाते रहने वाले प्रायः निराश असफल ही रहते देखे गये हैं।
आत्मिक प्रगति की दिशा में अभीष्ट सफलता प्राप्त करने वालों का इतिहास आदि से अन्त तक एक ही तथ्य प्रमाणित करता है कि उनने आवश्यक तपश्चर्या करके अपनी पात्रता विकसित की फलतः उन्हें विभूतियों, सिद्धियों से लाभान्वित होने का अवसर मिला। महामानवों से लेकर ऋषि महर्षियों तक की सफलतायें पूर्णतया उनकी तप साधना पर निर्भर रही है। मन्त्राराधन जादूगरी नहीं है। उसके पीछे प्रचण्ड तपश्चर्या की शक्ति ही चमत्कार प्रस्तुत करती है।
यथार्थता यह है कि भौतिक क्षेत्र की तरह ही आत्मिक क्षेत्र में भी आत्मपरिष्कार के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। उन्हीं के आधार पर वह क्षमता विकसित होती है जो अन्तर्जगत की प्रस्तुत दिव्य क्षमताओं को जगाकर किसी को विभूतिवान् बना सके। इसी आधार पर देवी अनुग्रह भी आकर्षित किये जाते हैं। वृक्षों का चुम्बकत्व बादलों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें पानी बरसाने के लिए विवश करता है। धातुओं की खदानें भी इसी आधार पर बनती और बढ़ती हैं कि जमा हुआ धातु भण्डार अपनी आकर्षण क्षमता से दूर-दूर तक फैले हुए सजातीय कणों को खींचता रहता है और उनके खिच-खिंचकर जमा होते रहने से खदान का आकार भण्डार बढ़ता रहता है। फूल खिलता है तो भौंरे प्रशंसा करने, मधुमक्खी याचना करने और तितली शोभा बढ़ाने के लिए अनायास ही जा पहुंचती हैं। अच्छे डिवीजन से पास छात्रों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश पाने तथा छात्रवृत्ति मिलने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। प्रतिभावानों को उनकी योग्यता के अनुरूप, पद, धन और मान अनायास ही मिलता जाता है। यही बात सिद्धान्ततः आत्मिक प्रगति की दिशा में अक्षरशः लागू होती है। साधक की पात्रता का विकास जिस अनुपात से होता है उसी क्रम में उसका वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। इन दिव्य उपलब्धियों का उद्गम अन्तः क्षेत्र में भी है और व्यापक ब्रह्म सत्ता से भी अजस्र अनुग्रह बरसते हैं। दोनों ही क्षेत्रों की उपलब्धियों से साधक निहाल होता है। इतने पर भी मूल तत्व जहां का तहां है। जो पाना है उसका मूल्य चुकाया जाना चाहिए। कुछ में तो इस संसार में कुछ भी मिलने का नियम नहीं है। जो पाया है जो पाना है उसका मूल्य पहले या पीछे चुकाने की बात को किसी भी प्रकार झुठलाया नहीं जा सकता।
मूल्य देकर खरीदने का सिद्धांत ही सही और सनातन है। घटिया चीजें स्वल्प मूल्य में और बढ़िया वस्तुएं महंगे दाम पर खरीदी जाती हैं। असली हीरा हजारों में और नकली थोड़े से पैसों में बिकता है। मूल्य के अनुरूप ही उनका महत्व और सम्मान है। जीवित दुधारू गाय बहुत दाम की आती है किन्तु मिट्टी की छोटी सी गाय कम पैसे में मिल सकती है। सस्ते और महंगे का अन्तर स्पष्ट है। जीवित गाय, दूध, बछड़ा, गोबर आदि बहुत कुछ देती है किन्तु खिलौना गाय से मात्र मनोरंजन ही हो सकता है। सस्ती पूजा पत्नी से जिन सिद्धियों की अपेक्षा की जाती है वे यदि किसी को मिल भी सकें तो नकली ही होंगी। उनसे तरह-तरह के ध्यान दृश्य देखने जैसे कौतुक कौतूहल मात्र ही सम्भव हो सकते हैं। उतने भर से आत्म कल्याण की अथवा दूसरों की सहायता कर सकने जैसी अध्यात्म क्षमता किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती।
भौतिक जगत में पुरुषार्थ और उसके प्रतिफल का—कर्म और भाग्य का सिद्धान्त पग-पग पर चरितार्थ होता है। पुरुषार्थी सफलता पाते और शेखचिल्ली कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ते रहते हैं। आत्मिक क्षेत्र का पुरुषार्थ तपश्चर्या है। याचना की तिरछी तरकीबें नहीं। यदि पुरुषार्थ की—पात्रता की—शर्त न रही होती तो हर याचना करने वाले की मनोकामनायें सहज ही पूरी होते रहने की परम्परा पाई जाती। तब किसी को पुरुषार्थ की कष्टसाध्य प्रक्रिया अपनाने की तनिक भी आवश्यकता न होती।
तथ्यों को समझा जा सके तो बहुमूल्य आत्मिक विभूतियों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुरुषार्थ करने का सिद्धान्त भी सहज ही समझ में आ जायगा। आत्मिक पुरुषार्थ का नाम तपश्चर्या है इसी मार्ग पर चलते हुए प्राचीनकाल के महान आत्मवेत्ता उच्चस्तरीय सफलता प्राप्त कर सकने में सफल हुए हैं। भागीरथ का गंगावतरण—पार्वती का शिव वरण तप साधना से ही सम्भव हो सका था। तपस्वी दधीचि की अस्थियों से ही व्यापक असुर साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला वज्र बना। ध्रुव को परम पद तप से ही मिला। सप्त ऋषियों को उच्चस्तरीय गरिमा इसी आधार पर प्राप्त हुई। विश्वामित्र ने इसी शक्ति के आधार पर नई दुनिया बनाने का साहस किया था। परशुराम का तप ही उनके कुठार के रूप में संसार भर के अनाचार से लड़ सकने की क्षमता बनकर प्रकट हुआ था। शृंगी ऋषि के तप बल से ही उनकी मन्त्र शक्ति इतनी समर्थ हो सकी कि उनके आचार्यत्व में किया गया दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ सार्थक हो सका। मध्यकाल में भी भगवान बुद्ध से लेकर योगी अरविंद तक की परम्परा में तपश्चर्या ही प्रधान रही है।
असुर वर्ग की क्षमतायें भी तपश्चर्या के आधार पर ही उभरी थीं। पुराण साक्षी है कि हिरण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, मेघनाद, मारीच, वृत्तासुर, भस्मासुर, सहस्रबाहु असुरों ने प्रचण्ड सामर्थ्य तप के बल पर ही प्राप्त की थी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कितने ही नर-नारी तप साधना के सहारे उच्चस्तरीय आत्मशक्ति का सम्पादन कर सके हैं। गान्धारी ने नेत्र शक्ति, समय की दिव्य दृष्टि, कुन्ती की देव सन्तान, सुकन्या का पति की वृद्धता निवारण, सावित्री का यम संघर्ष, अनुसुइया द्वारा तीन देवों को बाल स्वरूप जैसे घटनाक्रमों में तप की क्षमता ही उभरती हुई दिखाई पड़ती है। लोक हित के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकने वाले महामानवों में विलक्षण क्षमता का विकास साधना शक्ति के सहारे ही हो सका था। चाणक्य, समर्थ रामदास, गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस आदि के द्वारा लोक हित के जो महत्वपूर्ण काम बन पड़े उसमें उनके तपस्वी जीवन की गरिमा प्रकट होती है। तप साधना के स्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकने पर उन सब में व्यक्तित्व को पवित्र परिष्कृत, प्रखर बनाने वाली कष्टसाध्य जीवनयापन प्रक्रिया का समावेश तो निश्चित रूप में ही रहेगा। सरलतापूर्वक, स्वल्प श्रम में पूजा-पाठ करके ईश्वर अनुग्रह और आत्मोत्कर्ष का लाभ किसी को भी नहीं मिल सका है। भगवत् भक्ति भावुकता मात्र नहीं है। जीवनयापन की रीति नीति में आदर्शवादिता के लिए कष्ट सहन करने की नीति का समावेश किए बिना उपासना का मूल प्रयोजन पूरा ही नहीं होता। जहां वास्तविकता न होगी वहां प्रखर प्रतिफल भी कहां से प्राप्त होगा। सम्पन्नता, विद्वता, बलिष्ठता, प्रतिभा कलाकारिता, जैसी भौतिक सम्पदायें प्राप्त करने के लिए जब पुरुषार्थ करना पड़ता है तो इन सबसे अत्यधिक मूल्यवान आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए तप साधना से बच कर कोई सस्ती सरल पगडण्डी कैसे निकल सकती है। आत्मिक प्रगति का राजमार्ग तपश्चर्या के बलबूते पर ही पार किया जाता है।
गृह त्याग आवश्यक नहीं :—
आवश्यक नहीं कि हर किसी को घर छोड़कर वनवास में रहने या कठोर कष्टसाध्य उपचारों को ही अपनाना अनिवार्य हो। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए—विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैसी कठोरता अपना सकना सम्भव होता है। इसके लिए संचित संस्कारों की और प्रचण्ड संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यह उच्चतम स्थिति है। आरम्भ छोटे से ही होता है। हर स्थिति का व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में भी तप साधना के सिद्धान्तों का न्यूनाधिक मात्रा में समावेश कर सकता है और उतने से भी आनुपातिक लाभ उठाता रह सकता है।तप का तात्पर्य है गर्मी उत्पन्न करना। गर्मी रगड़ से उत्पन्न होती है। घर्षण ही ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। बिजली बनने से लेकर आग जलने तक समस्त प्रकार के ऊर्जा उत्पादनों का स्रोत घर्षण ही है। श्वास-प्रश्वास क्रिया की प्रतिक्रिया ही शरीर को जीवित रखने वाली गर्मी बनाये रहती है। तप का तात्पर्य है पशु प्रवृत्तियों के विरुद्ध दैवी प्रकृति का टकराव उत्पन्न कर देना। इसी संघर्ष से अध्यात्म क्षेत्र की वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे तप शक्ति के नाम से जाना जाता है। महान आध्यात्मिक प्रयोजन इसी शक्ति के सहारे सम्पन्न होते हैं। समुद्र मंथन से चौदह रत्न निकलने की कथा प्रसिद्ध है। जीवन मन्थन से भी इसी प्रकार का विभूति उत्पादन होता है।
पशु प्रवृत्तियों का निराकरण और उनके स्थान पर दैवी सत्प्रवृत्तियों का प्रतिष्ठान। यही है उपासना का—साधना का—योग साधना का—तपश्चर्या का एक मात्र उद्देश्य। आध्यात्मिक क्षेत्र की समस्त सफलतायें एक इसी केन्द्र पर केन्द्रीभूत हैं। सिद्धियों का उद्गम स्रोत यही है। इस क्षेत्र में जागृति एवं प्रगति उत्पन्न करने के लिए तपश्चर्या की जाती है।
नरक से निकाल कर स्वर्ग में पहुंचाने की क्षमता एकमात्र तपश्चर्या में ही है। इसलिए मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को तपस्वी बनाया था। विनोबा की माता भी अपने तीनों बालकों को ब्रह्मज्ञानी ब कर अपने परिवार को देवोपम सम्मान दिला गई। तप से स्वर्ग मिलता है। इस तथ्य के समर्थन में असंख्यों शास्त्र वचन और पौराणिक उपाख्यान उपलब्ध हैं। महामानवों की समूची बिरादरी वस्तुतः तपस्वियों की ही देव सेना है। उनमें से प्रत्येक ने अपनी पशु प्रवृत्तियों के साथ—दैवी आदर्शवादिता का संघर्ष कराया है। सामान्य लोगों पर स्वार्थांधता, भोग-लालसा और वासना-तृष्णा ही छाई रहती है जबकि महामानव दैवी परम्पराओं को इस प्रखरता के साथ अपनाते हैं कि उसके सम्मुख पशुता को परास्त होते और पलायन करते ही देखी जा सके। स्वार्थ-परमार्थ के संघर्ष में कौन विजयी होता है? पशु और देवता में से कौन जीतता है? उसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि मानवी आकांक्षा और श्रमशीलता अपना समर्थन और योगदान किस पक्ष को प्रदान करती है। इस संदर्भ में आन्तरिक महाभारत होना निश्चित है। उस धर्मयुद्ध में जिसको जितना शौर्य साहस एवं त्याग बलिदान प्रस्तुत करना पड़े। उसे उसी स्तर का तपस्वी कहा जा सकता है। जिसने जितनी शक्ति एकत्रित कर ली समझना चाहिए आत्मिक प्रगति का—अपूर्णता को पूर्णता में परिणत करने का लक्ष्य उसके उतना ही समीप आ गया। तप ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। उसी के आधार पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। उसी के सहारे शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। इसी क्षमता को जो जितना उत्पन्न-उपलब्ध करले समझना चाहिए कि उसकी आन्तरिक सम्पन्नता उसी स्तर तक समुन्नत हो गई।
आत्मिक प्रगति का जिनने महत्व समझा हो उन्हें उस उपलब्धि का उचित मूल्य चुकाने का भी साहस उत्पन्न करना चाहिए। सिद्धियां सदा ही पुरुषार्थियों को प्राप्त रही हैं। विजय श्री शूरवीरों के ही हिस्से में आई है। आध्यात्मिक क्षेत्र का शौर्य साहस—पौरुष पराक्रम तप साधना के रूप में ही जाना जाता है। यहां एक बात पूरी तरह स्मरण रखी जानी चाहिए कि अकारण काय कष्ट देने को नहीं—उच्चस्तरीय आदर्शों के परिपालन में शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना आवश्यक है इसी को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तप साधन कहलाता है।
प्रभु के साझेदार बनें—
पृथ्वी और सूर्य की साझेदारी से ही अपने संसार की गतिविधियां चल रही हैं। शरीर और चेतना का पारस्परिक सहयोग ही जीवन है। नर नारी की सघनता से गृहस्थ बनता है। यह साझेदारी यदि परमात्मा के साथ स्थापित कर सकने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति साहस कर सके तो समझना चाहिए कि उसके जीवन व्यवसाय में असीम लाभ मिलने की व्यवस्था बन गई।सुयोग्य, सफल और समर्थ लोगों के साथ मिल जुलकर रहने में बुद्धिमानी ही बुद्धिमानी है। चन्दन के समीप उगने वाले अन्य पौधे भी सुगन्धित हो जाते हैं। पारस और लोहे के स्पर्श से सोना बनने की बात प्रसिद्ध है। सत्संग की महिमा इतनी बढ़ी चढ़ी हो तो सघन समन्वय की महिमा उससे भी अधिक क्यों न होगी। ईश्वर निश्चित रूप में इस योग्य है कि उसके साथ बिना आगा पीछा सोचे जीवन व्यवसाय में साझेदारी की जा सकती है। इसमें ऐसा कोई जोखिम नहीं है जिसके लिए आरम्भ से असमंजस और अन्त में पश्चाताप करने की आवश्यकता पड़े।
भिक्षुक एकांगी होता है याचना से उसका स्तर गिरता है और तिरस्कार पूर्वक थोड़ा सा ही मिलता है। किन्तु मित्र, साथी, उत्तराधिकारी अथवा भागीदार की स्थिति दूसरी ही होती है। वह अधिकार और सम्मान पूर्वक अपने लिए उपयुक्त सुविधा प्राप्त कर लेता है। किन्तु स्मरण रहे साझेदारी के कुछ सिद्धान्त हैं। न्याय और नीति अपनाये रहने पर ही वह साझेदारी चलती है।
जीवन व्यवसाय में शरीर और आत्मा दोनों की ही साझेदारी है। इस कारखाने को चलने में दोनों की ही पूंजी और मेहनत लगती है। अस्तु आत्मा का भाग अधिक और शरीर का कम है। शरीर जड़ है। उसे मात्र औजार उपकरण, बाह्य सेवक की संज्ञा मिल सकती है। वह मशीन की तरह कार्य करता है। जीवन का सारा कारखाना आत्मा की चेतना और क्षमता पूंजी के सहारे चल रहा है। वह हाथ हटाले तो काया में तत्काल सड़न आरम्भ हो जायगी और जल्दी से जल्दी गाढ़ने, जलाने, बहाने आदि का प्रबन्ध करना होगा। व्यक्तित्व गरिमा काया पर नहीं चेतना के स्तर पर अवलम्बित है। अस्तु महत्व भी उसी का अधिक है। ऐसी दशा में उपार्जन के लाभ का बड़ा अंश भी उसी को मिलना चाहिए।
पर होता ठीक उल्टा है। शरीर सब कुछ हड़प जाता है और आत्मा की आवश्यकता पूर्णतया उपेक्षित ही बनी रहती है। उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। पेट और प्रजनन की दोनों ही आवश्यकताएं शरीर की हैं। वासना की तृप्ति इन्द्रियां चाहती हैं। मन मस्तिष्क की ग्यारहवी इन्द्रियां शरीर का एक अवयव हैं। इसकी भूख लोभ मोह की तृष्णा और अहंता की पूर्ति मांगती है। शरीर और मन की कितनी ही आवश्यकताएं परिवार से पूरी होती हैं। इसलिए वह परिवार भी शरीर के विस्तार क्षेत्र में ही सम्मिलित है।
असंख्य योनियों में परिभ्रमण करने के उपरान्त मनुष्य जन्म का सुर दुर्लभ अवसर मिलता है। इसका प्रयोजन एक ही है कि अपूर्णता को पूर्णता में परिणत किया जाय। भव बन्धनों से छुटकारा पाया जाय। अगली कक्षा देवत्व को उपलब्ध किया जाय। ईश्वरीय भंडार की सबसे बड़ी सम्पदा मानवी काया है। इससे बढ़कर और मूल्यवान पदार्थ परमात्मा के भंडार में है ही नहीं। जो अन्य प्राणियों को नहीं मिली उन विशेषताओं से सम्पन्न विभूतिवान शरीर मौज करने के लिए नहीं वरन् धरोहर के लिए इस निमित्त दिया है कि उससे विश्व उद्यान को अधिक समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान दिया जाय—हाथ बटाया जाय। इन प्रयोजनों की जितनी पूर्ति जीवन सम्पदा से हो सके समझना चाहिए आत्मा को उतना ही लाभांश मिला। जितना पेट प्रजनन के लिए लग गया उतना शरीर की भागीदारी में चला गया माना जाय। देखते हैं कि इस दृष्टि से आत्मा को घाटा ही घाटा है। शरीर की लिप्साएं पूरी करने के लिए अनेकों कुकृत्य तक करने पड़ते हैं। मरने पर शरीर तो श्मशान में समाप्त हो जाता है पर उन कुकर्मों का फल आत्मा को जन्म जन्मान्तरों तक दुर्गति सहने के रूप में भुगतना पड़ता है। बुद्धिमान बनने वाला मनुष्य जीवन के स्वरूप, मूल्य, उद्देश्य और उत्तरदायित्व को समझने में कितना मूर्ख सिद्ध होता है। इस विसंगति को देखते हुए भारी आश्चर्य होता है।
आत्म ज्ञान, आत्म बोध आत्म साक्षात्कार उस जागृति को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने स्वरूप और लक्ष्य को समझ सकने योग्य बन सके। जिस विवेक बुद्धि से आत्मा की स्थिति और प्रगति का निर्धारण कर सकना संभव होता है उसे ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। मनुष्य जीवन के उपरान्त ईश्वर का दूसरा अनुग्रह यही है। किन्तु यह मिलता उसी को है जो आत्म कल्याण की महत्ता और आवश्यकता समझता है जिसे मोह मदिरा की खुमारी छाई हुई है उसके लिए न इस अनुकम्पा की आवश्यकता है और न उपयोगिता। ऐसे कुपात्रों को ऋतम्भरा प्रज्ञा का—गायत्री महा शक्ति का—अनुग्रह वरदान मिले भी तो कैसे? ब्रह्मविद्या का प्रत्येक सोपान अपने आपको जानने, आत्म कल्याण में लगने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है—शरीर का ही नहीं आत्मा का भी महत्व समझा जाय और सब कुछ शरीर पर ही निछावर न किया जाय कुछ तो आत्मा के लिए सोचा जाय।
बुद्धिमानी इसमें है कि जीवन में आत्मा और शरीर की साझेदारी को स्वीकार किया जाय। और उपलब्धियों का विभाजन दोनों की आवश्यकता के अनुरूप किया जाय। शरीर की आवश्यकताएं स्वल्प हैं थोड़े समय में थोड़े परिश्रम से पेट भरने के साधन जुटाये जा सकते हैं। परिवार यदि सीमित रखा जाय। औसत भारतीय के स्तर तक उसकी आवश्यकताएं पूरी करने में संतोष रखा जाय तो वह निर्वाह भी थोड़ा सा समय और मनोयोग लगाने पर सहज ही पूरा होता रह सकता है। शरीर की आवश्यकताएं यदि इतनी ही मान ली जायं। उनकी पूर्ति में संतोष कर लिया जाय तो फिर आत्मा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन बच सकते हैं। भौतिक महत्वाकांक्षाएं सीमित किये बिना आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो सकती
यह एक सुनिश्चित तथ्य है।
आत्मा की आवश्यकता पूरी करने के लिए सुसंस्कार संवर्धन के लिए प्रयत्न करने चाहिए। सत्प्रवृत्तियों के सम्वर्धन से ही आत्मा की बल वृद्धि होती है। आत्म परिष्कार और आत्मिक प्रगति एक ही बात है। इसके लिए कुसंस्कारों का उन्मूलन एवं सुसंस्कारों का संस्थापन आवश्यक होता है। यह सफलता चार साधनाओं के सहारे मिलती है। जिन्हें साधना, स्वाध्याय, संयम सेवा के चार आत्म पुरुषार्थों के रूप में बताया गया है। इन चारों के लिए समय, श्रम और मनोयोग एवं संकल्प शक्ति का आवश्यक अंश लगे तो ही उनकी वास्तविक पूर्ति हो सकती है। चिन्ह पूजा की लकीर पीटने भर से तो कुछ बनता नहीं है।प्रभु समर्पित जीवन से परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है समर्पण बड़ी बात है शरणागति में अपना कुछ बचता ही नहीं। सब कुछ उसका हो जाता है जिसको समर्पण किया है इसका स्वरूप समझना हो तो नाले का नदी में, ईंधन का आग में, पानी का दूध में, बूंद का समुद्र में, पतंगे का दीपक में, पति का पत्नी में विलय होते देखकर यह जानना चाहिए कि शरणागति की स्थिति में भक्त और भगवान का एकत्व अद्वैत किस स्तर का होता होगा। तब भक्त की अपनी कामना ही नहीं सत्ता भी समाप्त हो जाती है। और काया पर, मन पर, अन्तःकरण पर पूरी तरह इष्ट देव का ही अनुशासन छाया रहता है। इस स्थिति में पहुंचने पर भक्त भगवान एक हो जाते हैं दोनों की सत्ता में नाम मात्र का ही अन्तर रह जाता है।
समय श्रम की सम्पदा क्रिया रूप में और मन बुद्धि की विभूति चिंतन रूप में उपलब्ध है। इन दोनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाय तो शरीर की ही तरह आत्मा को भी अपनी आवश्यकतायें पूरी करने में इनका लाभ मिलता रहे। समय 24 घण्टे का होता है। इसमें सोने के लिए सात घण्टे आजीविका उपार्जन के लिए आठ घण्टे, अन्य कार्यों के लिए पांच घण्टे इस प्रकार बीस घण्टे शरीर यात्रा के लिए लगाये जा सकते हैं। इतने घण्टों को यदि आलस्य प्रमाद में न गंवा स्फूर्ति और उत्साह का समावेश करते हुए काम किया जाय तो सामान्य निर्वाह का शारीरिक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का क्रम बहुत ही शान्ति सरलता और सुव्यवस्था के साथ चलता रह सकता है। तृष्णा का तो कहीं अन्त नहीं लोभ और मोह की पूर्ति तो 24 घण्टे से भी अधिक बड़ा दिन होने लगे और दिन रात उपार्जन उपयोग में ही संलग्न रहा जाता रहे तो भी पूर्ति नहीं हो सकती। औसत भारतीय स्तर का जीवन क्रम सन्तोषजनक मान लिया जाय तो इतने समय में सब कुछ भली प्रकार पूरा होता रह सकता है। शेष चार घण्टे परमार्थ प्रयोजनों में भली प्रकार लगते रह सकते हैं। मन और बुद्धि का उपयोग सत्प्रयोजनों के लिए खाली घण्टों में होता रहने में तो कुछ कठिनाई है ही नहीं। सामान्य काम काज करते समय भी चिंतन की उत्कृष्टता की परिधि में नियोजित किया जा सकता है। कामुकता को—ईर्ष्या द्वेष की पाप और पतन की विचारणाओं एवं योजनाओं के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं लगाना पड़ता। सामान्य काम काज करते, फुरसत रहते सोते ऊंघते वह कल्पनायें मस्तिष्क में दौड़ती रहती हैं। और उन्हीं क्षणों में वह सब कुछ परिपक्व हो जाता है जो अवांछनीयता अपनाने के लिए आवश्यक है। अश्लील चिन्तन के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं निकालना पड़ता। ठीक इसी प्रकार परमार्थ प्रयोजन के लिए निर्धारित चार घण्टों के अतिरिक्त सामान्य काम काज के बीच भी मन बुद्धि से आत्मकल्याण की कल्पनायें करने और योजनाएं बनाने का पर्याप्त अवसर मिल सकता है।
तीसरी सम्पदा है धन इसके उपार्जन का भी शरीर और आत्मा के बीच न्यायोचित विभाजन होना चाहिए। जीवन में ईश्वर की हिस्सेदारी मानी जाय तो धन वैभव का एक अंश भी उसके निमित्त अर्पण किया जाना चाहिए, यह अंश कितना हो यह व्यक्ति की उदारता और परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। यह फैसला अपने अन्तःकरण को पंच मानकर निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह स्वतः ही करना चाहिए। यों होता तो यह रहा है कि सारी कमाई वासना तृष्णा और अहंता की वैश्याएं ही लुभा फुसला कर अपहरण करती रहीं हैं। आत्मा के पल्ले तो भूसी भी नहीं पड़ती है। उस पुराने अनियत अभ्यास को घटाने छोड़ने में हीला हुज्जत तो बहुत होगी। घर परिवार वालों से लेकर मित्र हितैषी स्वजन सम्बन्धी होने का दावा करने वालों तक की इस सम्बन्ध में एक स्वर से असहमति होगी कि ईश्वर के लिए आत्म कल्याण के लिए-परमार्थ के लिए भी कोई कहने लायक अंश निकाला जाये। वे नकली सुपाड़ी, नकली अगरबत्ती, अक्षत, रोली जैसे चार पैसों के अनुदान से अधिक कुछ त्याग करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता से लेकर सम्बद्ध स्वजनों तक का सारा परिवार इस बात का विरोधी होगा कि जीवन सम्पदा में से श्रम, समय, मन, बुद्धि अथवा धन का साधन का कोई महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजन के लिए लगाया जाय।
इस मोह परिवार का तो उल्टा दबाव यह रहता कि ईश्वर से किस बहाने अधिक भौतिक लाभ पाने का जुगाड़ बिठाया जाय। ऐसी दशा में ईश्वर के निमित्त साधनों की भागीदारी प्रस्तुत करने के लिए तथा कथित अपनों की सहमति प्राप्त कर सकना निश्चय ही टेढ़ी खीर है।
जो हो आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए हिमाच्छादित पर्वत शिखर पर चढ़ने जितना साहस जुटाया जाना आवश्यक है। इस साहसिकता का आरम्भिक परिचय जीवन में ईश्वर की साझेदारी स्वीकार करने और लाभांश को दोनों भागीदारों में वितरित करने का निश्चय अपनाकर ही दिया जा सकता है।
इतना तो कर ही सकते हैं?
इस दिशा में कोई बड़ा साहस करते न बन पड़े तो भी इतना तो करना ही चाहिए कि ईश्वर को—परमार्थ को अपने परिवार का एक नया सदस्य मान लिया जाय। प्रत्येक सदस्य पर जो औसत खर्च आता है उतना परमार्थ के लिए भी किया जाय। संतान के भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, स्वावलम्बन एवं उत्तराधिकार में जो खर्च किया जाता हो उतना ही ईश्वर रूप एक नई संतान के लिए भी खर्च करना आरम्भ कर दिया जाय। समझा जाय कि ईश्वरीय अनुकम्पा के रूप में—आत्म जागृति के रूप में एक सन्तान ने हमारे परिवार में जन्म लिया है और घर के अन्य सदस्यों की तरह घर की संचित सम्पत्ति तथा सामयिक आजीविका में अपनी भागीदारी का दावा प्रस्तुत किया है। न्याय की मांग है कि घर के किसी सदस्य को उसकी उचित भागीदारी के अधिकार से वंचित न किया जाय। परमात्मा को—आत्मा को जीवन व्यवसाय में हिस्सेदार मान लेने पर उस अर्थ साधनों का भी परमार्थ के लिए एक सुनिश्चित अंश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।इस साझेदारी का स्मरण दिलाने और न्यायोचित विभाजन का तकाजा करने के लिए युग निर्माण योजना की सदस्यता की प्रारम्भिक शर्त में अंशदान को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। उसका न्यूनतम अंश एक घण्टा समय और दस पैसा नित्य ज्ञानघट के लिए लगाते रहने की बात कही गई है। ज्ञानघट इसी प्रयोजन के लिए स्थापित कराये गये हैं। इस दिशा में ध्यान देकर हम ईश्वर को साझेदारी का सिद्धान्त स्वीकार करते हैं। उस स्वीकृति के ऊपर मुहर लगाने हस्ताक्षर करने के रूप में ही यह न्यूनतम अंश है। यह आरम्भ है अन्त नहीं। यह बीजारोपण है वृक्ष नहीं। जिस प्रकार प्रयत्न करने पर हर व्यक्ति चार घण्टे रोज-समय का छटा भाग परमार्थ प्रयोजनों के लिए लगा सकता है उसी प्रकार यदि परमार्थ को नई सन्तान के रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो उसके लिए भी अर्थोपार्जन का अंश लगा सकना कुछ भी कठिन प्रतीत न होगा। प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि अंशदान की दृष्टि से पिछले दिनों से जो उदारता बरती जा रही है उसकी अपेक्षा इस बसन्त पर्व से उसका अनुपात बढ़ा ही दिया जाय। जबकि यहां यदाकदा तो कुछ होता रहता है पर नियमितता नहीं बरती जाती, उन्हें किसी न किसी रूप में इस क्रम को नियमित बनाने और दिनचर्या में सम्मिलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानघट की स्थापना में और ज्ञान यज्ञ के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुदान प्रस्तुत करते रहने में तो किसी को कृपणता बरतनी ही नहीं चाहिए।
ईश्वर से मांगने की बात उचित है पर साथ ही दूसरा पक्ष यह भी सोचना चाहिए कि उसकी पात्रता सिद्ध करने को अपनी ओर से उदारता अपनाने की शर्त पूरी की गई या नहीं। समर्पण के अनुपात से अनुग्रह मिलने का तथ्य यदि हृदयंगम किया जा सके तो हम यथार्थता के अधिक निकट होंगे। समर्थों की साझेदारी में लाभ ही लाभ है। विश्व माता वेद माता ईश्वरीय दिव्य सत्ता को यदि साहस पूर्वक अपने जीवन व्यवसाय में साझीदारी बनाया जा सके तो इसे असाधारण लाभ कमाने और बुद्धिमान सिद्ध होने के राजमार्ग पर चल पड़ना ही कहा जायगा। इस बार का बसन्त पर्व हममें से प्रत्येक को इसी स्तर की साहसिकता अपनाने की प्रेरणा लेकर आया है। उसे जो जितनी मात्रा में अपना सकेंगे वे उतने ही दूरदर्शी सिद्ध होंगे।
***
*समाप्त*
*समाप्त*