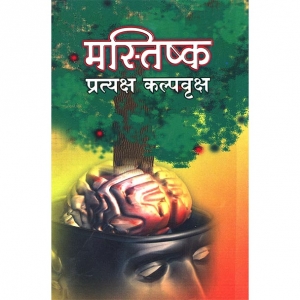मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष 
संतुलन साधें—सुखी निश्चिंत रहें
Read Scan Version
रोगों के आक्रमण को शरीर एक सीमा तक ही सह पाता है उसके बाद उसकी क्रियाशक्ति जवाब देने लगती है। यही कारण है कि शरीर में रोगों के चिह्न कभी दिखाई दें, उनके बीज पहले से पड़ते और उगते रहे हैं। मस्तिष्क के बारे में भी यही सच है। सामान्य आधियों को मस्तिष्क अपने आप ही ठीक करता और उनसे निबटता रहता है। उनसे निबटने की, स्वयं उपचार करने की सामर्थ्य मस्तिष्क में एक सीमा तक ही रहती है उसके बाद ही आत्म हत्या, पागलपन जैसे भयंकर रोगों के रूप में उनका विस्फोट होता है।
यों इन रोगों की प्रतिक्रिया में अकस्मात् ही उत्पन्न हुई मालूम पड़ती है पर वस्तुतः ये मनुष्य के मन में लंबे समय से चलती आ रही उधेड़बुन ताने बाने, चिंता व्यथा, परेशानी, उद्विग्नता और आवेश की भावनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मानसिक दुर्बलताओं के परिणाम स्वरूप ही आत्महत्या और पागलपन की घटनायें घटती है।
आत्म-हत्या के मोटे एवं प्रत्यक्ष कारणों में गृहकलह, मानहानि, पश्चाताप, परीक्षा आदि प्रयोजनों में असफलता, भविष्य की निराशा, दरिद्रता, असाध्य रोग, दण्ड भय, असफल प्रेम, आदर्शवादी दुस्साहस आदि कारण गिनाये जा सकते हैं। किन्तु उसका वास्तविक कारण एक ही है मनःक्षेत्र की ऐसी दुर्बलता जो विपरीत परिस्थितियों का तनिक-सा दौर आते ही भड़क उठती है और बेकाबू होकर अनर्थ के गर्त में जा गिरती है। दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति भी तनिक-सी ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। तनिक-सी सर्दी-गर्मी न सह सकने के कारण भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को धीरे-धीरे बिगाड़ते हुए लोग उस स्थिति तक जा पहुंचते हैं जहां आत्म हत्या दुर्घटना को अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता।
चिन्तन की सही पद्धति यदि समझी और समझाई गई होती तो स्थिति को सहन या सुधारने की अभीष्ट विधि-व्यवस्था अपनाने की आदत डाली गई होती और इन आत्म-हत्या करने वालों में से अधिकांश के प्राण बच सकते थे क्योंकि वस्तुतः जीवन सम्पदा को कूड़े-करकट के ढेर में फेंक देने को विवश करने वाली कोई भी विपत्ति इस संसार में है ही नहीं।
‘मैलन कोलिय’ के रोग विषादग्रस्त रहते हैं वे दुखी, असन्तुष्ट एवं क्षुब्ध रहने के लिए कोई न कोई कारण अपने इर्द-गिर्द ही ढूंढ़ लेते हैं। किसी न किसी को अपने दुःखद चिन्तन का पात्र चुन लेते हैं। वस्तुतः वे व्यक्ति या वे परिस्थिति विक्षोभ कारक उतने नहीं होते जितना कि उन्हें गढ़ लिया है।
‘रैप्टस मेनेकलिक्स’ उस सनक का नाम है जिनमें मनुष्य दण्ड देने के लिए आतुर रहता है, पर वह इसके लिए अपने आपको ही चुनता है। आत्म-प्रताड़ना के लिए इसकी इच्छा निरन्तर उठती है। भोजन न करने, कपड़े न पहनने सिर धुनने से लेकर आत्म-हत्या करने तक की चेष्टाएं वह करता है। कभी-कभी अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तक को तोड़-फोड़कर फेंक देता है। ऐसा करने से उसे अपने विक्षोभ का समाधान होने की बात सूझती है।
दूसरों के क्षोभ को शान्त करने के लिए स्वयं दुःखी होने की स्थिति अपना लेना भी ऐसा ही विचित्र चिन्तन है जिसे अक्सर सहानुभूति एवं सहायता के लिए अपनाया जाता है। किसी स्वजन के कष्ट निवारण के लिए अपने आप की बलि किसी देवी-देवता पर चढ़ा देना अथवा विवाह योग्य कन्याओं का इसलिए आत्मघात कर बैठना कि इससे उनके अभिभावकों को अर्थचिंतन से छुटकारा मिल जायगा—ऐसे ही दुस्साहस भरे कदम हैं। इनमें आदर्शवाद, उदारता, सहानुभूति जैसे तत्वों का पुट तो होता है, पर यह स्मरण नहीं रहता कि इस कदम से अपना बहुमूल्य जीवन ही नष्ट नहीं होगा वरन् जिनके लिए यह सब किया जा रहा है उनकी कठिनाई, चिन्ता एवं विपत्ति और अधिक बढ़ जायगी।
प्राचीनकाल में आत्मघात को धार्मिक प्रशंसा प्रदान करने का भी कभी-कभी प्रचलन रहा है। इसके पीछे भारत की मूल संस्कृति नहीं वरन् सामयिक विचार विकृति ही झांकती है। संन्यासियों की स्वाभाविक मृत्यु की अपेक्षा स्वेच्छा मरण की प्रशंसा की गई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसे विधान भिक्षुजनों के लिए उनके धर्म-ग्रन्थों में मिलते हैं, भले ही वे पीछे जोड़े गये हैं। पाण्डवों का स्वर्गारोहण, मंडन मिश्र का तुषाग्नि संदाह, ज्ञानेश्वर की जीवित समाधि आदि अनेक ऐसी घटनाएं इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं, जिन्हें सराहा ही जाता है। चित्तौड़ की रानियों का सामूहिक रूप से आत्मदाह और मृत पतियों के साथ अनेक पत्नियों का सती हो जाना ऐसे ही कृत्यों में गिना जाता है जिसके लिए उन्हें प्रशंसा योग्य ठहराया जाय।
इतिहास पुराणों में ऐसे अनेकों घटना प्रसंग उपलब्ध हैं जिनमें कतिपय नर-नारियों ने धार्मिक प्रयोजनों के लिए अथवा दूसरों की तुलना में अपने को अधिक आदर्शवादी, अधिक साहसी सिद्ध करने के लिए आत्मघात किये हैं। पराजित एवं असफल लोगों द्वारा प्राण त्याग करके अपनी ग्लानि मिटाने की घटनाएं तो सदा ही होती रही हैं। उन्हें लोगों ने सराहा तो नहीं, पर सहानुभूति की दृष्टि से अवश्य देखा। मृतकों के लिए यह सहानुभूति चिन्तन भी प्रेरक बना। आत्मघात का साहस न कर सकने पर अपनी सन्तान की अथवा पशु-पक्षियों की बलि चढ़ा देने की प्रथा तो एक प्रकार से किसी काल में मान्यता प्राप्त धर्म कृत्य बन गई थी और कहीं-कहीं अभी तक उसका प्रचलन मौजूद है।
आत्म-हत्या को भी दूसरों की हत्या के समान ही गर्हित कर्म माना जा सकता है। प्राचीनकाल में इसे बहुत बुरा कहा जाता था और मरने के उपरान्त भी इस कुकृत्य करने वाले की भर्त्सना की जाती थी।
योरोप में उन दिनों आत्म-हत्या करने वालों के प्रति बहुत अनुदार दृष्टिकोण था। उनकी लाशें सड़कों के आस-पास कूड़े के ढेर में दबादी जाती थीं और भयंकर आकृतियां वहां खड़ी कर दी जाती थीं, ताकि उन मरने वालों की बदनामी हो। इन परिस्थितियों को बदलने में डेविडह्यूम, वाल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने आवाज उठाई थी और कहा था, आदमी को जीने की तरह मरने की भी आजादी होनी चाहिए।
कुरान में दूसरों की हत्या करने से भी अधिक जघन्य पाप आत्म-हत्या को बताया है। यहूदी धर्म में भी ऐसा ही है, उसमें आत्म-हत्या करने वाले के लिए शोक मनाने और उसकी आत्मा को शान्ति देने के लिए प्रार्थना करने की भी मनाही है। ईसाई धर्म में भी इसे घृणित पातक बताया गया है। 11 वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में एक कानून बना था, जिसमें आत्म-हत्या करने वाले की सम्पत्ति जब्त करली जाती थी और उसके शव को किसी ईसाई कब्रिस्तान में धार्मिक विधि से दफनाया नहीं जा सकता था।
आत्म-हत्या का प्रयत्न करने वाले को रोगी माना जाय या अपराधी? इस प्रश्न के उत्तर में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे लोगों का उचित स्थान जेलखाना नहीं, वरन् पागलखाना है। भारत सरकार की मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति को तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा0 सुशीला नैयर ने सुझाव दिया था कि आत्महत्या की चेष्टा एक मानसिक विकृति है इसलिए इस प्रकार का प्रयत्न करने वालों को अपराधी नहीं वरन् रुग्ण व्यक्ति माना जाना चाहिए। अब इंग्लैण्ड के कानूनों में भी इस सन्दर्भ में सुधार कर लिया गया है उन्हें दण्डनीय नहीं माना जाता।
पागलपन भी मानसिक दुर्बलता के कारण उत्पन्न होने वाली मनोव्याधि है। अब तक इस रोग का विद्युतीय उपचार किया जाता है पर पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने इन रोगों का अन्य उपायों से उपचार करने की विधि भी खोज निकाली है।
मनोरोगों का प्रेमोपचार
विश्व विख्यात मनःशास्त्री टामस मैलोन ने पागलपन के कारण ढूंढ़ने वाले अनेकों शोध संस्थानों का मार्गदर्शन किया है और उन्हें परीक्षणों के आधार पर किसी उपयुक्त निष्कर्षों तक पहुंचाने में सहायता की है। उनके अनुसन्धानों के निष्कर्षों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह पाया है कि ‘मनुष्य दूसरों का प्यार पाना चाहता है; पर वह उसे मिल नहीं पाता। इस अभाव से उसके अन्तःक्षेत्र की गहरी परतों में निराशा जन्य उदासी छा जाती है। फलतः उसका चिन्तन प्रवाह अपना सीधा रास्ता छोड़कर भटकावों में फंस जाता है। प्यार पाने की असफलता का कारण सम्भव है उस व्यक्ति के अपने ही दोष दुर्गुणों में रहा हो, पर इससे क्या, उसकी आकांक्षा तो अतृप्त ही रह गई। वह यह समीक्षा कहां कर पाता है कि दोष अपना है या पराया। भोजन किसी भी कारण न मिले, पेट का विक्षोभ तो हर हालत में रहेगा ही। इसी प्रकार प्यार के अभाव में मनुष्य अपना मानसिक सन्तुलन धीरे-धीरे खोता चला जाता है और एक दिन स्थिति वह आ जाती है जिसमें उसे विक्षिप्त एवं अर्द्ध-विक्षिप्त के रूप में पाया जाता है।
जो पूर्ण विक्षिप्त हो चुके हैं उनकी बात दूसरी है, पर जो दूसरों के मन और व्यवहार का अन्तर समझने में किसी सीमा तक समर्थ हैं उनके रोग को साध्य माना जा सकता है। अधिक से अधिक यह समझा जा सकता है कि उपचार कष्ट साध्य है, पर असाध्य तो नहीं ही कहना चाहिए। ऐसे रोगियों का उपयुक्त उपचार यह है कि उन्हें उपेक्षा के वातावरण से निकाल कर स्नेह-सद्भाव का अनुभव करने दिया जाय। जिनसे उसका वास्ता पड़ता है वे सभी उसे प्यार और सम्मान प्रदान करें। वैसा न करें जैसा कि आमतौर से पागलों के साथ किया जाता है। अटपटेपन पर खीज आना स्वाभाविक है, पर हितैषियों को यह मानकर चलना चाहिए कि रोगी आखिर रोगी है और उसके अटपटे व्यवहार जान-बूझकर की गई उद्धतता नहीं वरन् चिन्तन तन्त्र के गड़बड़ा जाने की विवशता भर है। ऐसी दशा में वह तिरस्कार एवं प्रताड़ना का नहीं, दया और दुलार का अधिकारी है।
प्यार की प्यास मानवी चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। पदार्थों के संग्रह इन्द्रियों की रसानुभूति के उपरान्त तीसरी भूख स्नेह की है जो व्यवहार में सम्मान के रूप में देखी जाती है। यश कामना उसी का रूप है। प्रतिष्ठा प्राप्त करते समय मनुष्य सोचता है कि यह सम्मान कर्ताओं द्वारा दिया गया स्नेह सद्भाव है। यों होता यह भ्रम ही है किन्तु असली न मिलने पर नकली से भी बहुत करके काम चलाते रहा जाता है। स्नेह के साथ सम्मान रहेगा किन्तु सम्मान का प्रदर्शन सदा स्नेह युक्त ही हो यह आवश्यक नहीं। उसमें छद्म भी घुला रह सकता है। सम्मान और यश के लिए लालायित प्रायः सभी पाये जाते हैं और उसके लिए समय, श्रम एवं धन भी खर्च करते हैं। यश लालसा के पीछे वस्तुतः प्यार को उपलब्ध करने की आकांक्षा ही काम करती है। लोग बड़प्पन के प्रदर्शन में उसे खरीदने की विडम्बना रचते रहते हैं।
पानी की प्यास से गला सूखता है और भूख से पेट उठता है। प्यार के अभाव में आदमी थकता नहीं टूटता भी है। एकाकीपन यों अन्य प्राणियों को भी सहन नहीं, पर मनुष्य के लिए तो वह ढोया जा सकने वाला भार है। वह साथ रहना ही नहीं चाहता ऐसे साथी भी चाहता है जो उसके अन्तस् को छूने, गुदगुदाने खड़ा रखने और उठाने में सहायता कर सकें। प्यार का अभाव अखरता तो धैर्यवानों को भी है, पर हलकापन तो उसके कारण उखड़ ही जाता है। प्रायः आन्तरिक उखड़ापन ही पगलाने की व्यथा बन कर सामने आती है। यों पागलपन के इसके अतिरिक्त भी और भी कितने ही कारण होते हैं।
इस प्रकार पगलाने वालों का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि वे प्यार की प्रकृति को नहीं जानते और यह नहीं समझ पाते कि यह अपने भीतर से निकलने वाली आभा भर है जो जहां भी पड़ती है वहां दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक चमक उत्पन्न करती और आकर्षक लगती है। अपना प्यार ही दूसरों में प्रतिबिंबित होता है। यदि उसमें कमी हो तो दूसरों का वास्तविक सद्भाव भी ठीक तरह समझ सकना सम्भव न हो सकेगा। इसके विपरीत अपनी प्रगाढ़ आत्मीयता होने पर साथियों का सामान्य शिष्टाचार भी गहरे दुलार की अनुभूति करता रहता है। बल्ब स्वयं जलता है और अपने क्षेत्र को प्रकाशवान करता है। व्यक्ति का अपना प्यार ही है जो विकसित होने पर दूसरों में प्रेम प्रतिदान मिलने के रूप में विदित होता रहता है।
जो इस तथ्य को समझते हैं वे पगलाने से बचे रहते हैं। चपेट में आते हैं तो अपना उपचार आप कर लेते हैं। दूसरों की प्रतीक्षा न करके अपनी ओर से सद्भाव बढ़ाते हैं और उसे साथियों में, सम्पर्क क्षेत्र में उसका प्रतिबिम्ब देखते हैं। मानसिक अवसाद का यह अति सरल किन्तु अत्यन्त कारगर स्वसंचालित उपचार है, पर दुर्भाग्य यह है कि इस तथ्य को कोई-कोई ही समझ पाते हैं। और अपनी ओर न देखकर स्नेह, सद्व्यवहार एवं सम्मान के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। न मिलने पर खीजते और दूसरों पर ही कृपणता, कृतघ्नता आदि का दोष लगाते हैं। सहयोग के अभाव में सांसारिक कामों में हानि पड़ने की बात सर्वविदित है। आन्तरिक सद्भावों की उपलब्धि भी उससे भी बड़ी आवश्यकता है। इतने बड़े उपार्जन का यही सरल उपाय है कि अपनी ओर से प्यार का प्रकाश फेंककर दूसरों को प्रिय पात्र बना लिया जाय और अपने ही प्रेम प्रकाश का आलोक समीपवर्ती क्षेत्र में छाया देखा जाय।
मानसोपचार की कठिनाई यह होती है कि वह पगलाये हुए रोगियों को यह दार्शनिक तथ्य समझा सकने में सफल नहीं हो पाते, समझने में तथाकथित समझदार भी असफल रहते हैं। मानसिक रोगी पहले तो अपनी विपन्नता ही स्वीकार नहीं करता, करता भी है तो उसे दूसरों की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई मानता है। जब तथ्य को स्वीकार ही नहीं किया गया तो उसके परिवर्तन के लिए बताया गया उपाय भी किस तरह गले उतरेगा। कदाचित ही कोई मनोरोग चिकित्सक अपने रोगियों को यह समझा सकने में सफल हो पाते होंगे कि उन्हें अपने भीतर आशा का, उल्लास का, प्रेम का स्रोत उभारना चाहिए और अपने सूखे मनःक्षेत्र को हरा-भरा कर लेना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है कि दो वयस्क मस्तिष्क लाख प्रयत्न करने पर भी उस तथ्य को समझने और समझाने में सफल नहीं होते, जिन पर कि उनकी प्रसन्नता और सफलता निर्भर है। जो हो, उपचार तो करना ही ठहरा। ऐसी दशा में एक ही उपाय शेष रह जाता है कि विक्षिप्तता एवं अर्ध विक्षिप्तता के रोगी से सहानुभूति रखने वाले सभी लोग अपना व्यवहार बदल लें। स्नेह, सहयोग और सम्मान का प्रदर्शन करें। आत्मीयजन होने के नाते यदि ऐसा सहज स्वाभाविक रूप से बन पड़े तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, पर यदि भीतर से वैसी उमंग न उठतीं हो तो भी प्रेम प्रदर्शन को कारगर उपचार मानकर उसके लिए आवश्यक प्रयास किया जाना चाहिए।
मानसोपचार में औषधियों का—विद्युत प्रयोगों का तथा अन्यान्य क्रिया-प्रक्रियाओं का भी महत्व है, पर उन सबके संयुक्त परिणाम में भी अधिक लाभदायक यह होता है कि पगलाये रोगी को स्नेह दुलार के वातावरण में रहने का अनुभव होने लगे। उद्धत मनोरोगियों की आक्रामक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने एवं सामान्य शिष्टाचार खो बैठने पर प्रतिबन्धित भी किया जाता है और वैसा करने से उसे क्या हानि उठानी पड़ेगी इसका अनुभव भी कराना चाहिए। अन्यथा उद्धत आचरण बढ़ता ही जायगा। इतने पर भी यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि मानसिक रोगों के रूप में जीवन की नाव में जो पानी घुसता है उसके प्रवेश द्वारा को प्यार के अभाव की अनुभूति ही कहा जा सकता है। अवसाद को उत्साह में बदल देना ही मानसिक रोगों की कारगर चिकित्सा है। इसमें प्रेमोपचार को जितनी सफलता मिलती है उतनी और किसी प्रयोग को नहीं। पहले कभी समझा जाता रहा था कि सोच समझ, विचार और सूझ बूझ मस्तिष्क का काम है—तथा भावनायें-संवेदनायें हृदय का। लेकिन यह धारणा कई वर्षों पहले गलत सिद्ध हो चुकी हैं और भावनाओं का क्रीड़ाक्षेत्र भी मस्तिष्क ही माना जाने लगा है। मानव मस्तिष्क के इस भाग को और अभी बहुत कम ही स्थान दिया गया है। इस भावनात्मक मस्तिष्क के खोज का कार्य अभी नितान्त आरम्भिक अवस्था में ही माना जा सकता है। मस्तिष्क के भीतर मोटी और काफी लम्बाई तक फैली हुई अन्तस्त्वचा के भीतर विशिष्ट प्रकार की तन्त्रिकाएं फैली हुई हैं। यद्यपि यह मस्तिष्क के प्रचलित वर्गीकरण में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकती हैं तो भी यह देखा जाता है कि सुख, दुख, भय, हर्ष, क्रोध, आवेश, करुणा, सेवा-स्नेह, कामुकता, उदारता, संकीर्णता, छल, प्रेम, द्वेष आदि भावनाओं का इसी स्थान से सम्बन्ध है। और ये भावनाएं ही हैं जो चेतन ही नहीं अचेतन मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। इच्छा संचालित और अनिच्छा संचालित केन्द्रों में भारी उलट पुलट प्रस्तुत करती हैं।
कुछ दिन पहले शारीरिक आवश्यकतानुसार मानसिक क्रियाकलाप की गतिविधियों का चलना माना जाता था। भूख लगती है तो पेट भरने की चिन्ता मस्तिष्क को होती है और पैर वैसी सुविधा वाले स्थान तक पहुंचते हैं जहां हाथ खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। मुंह चबाता है और पेट पचाता है। इसी प्रकार आहार के उपरान्त निद्रा, विश्राम के लिए, छाया घर निवास की—शैया, बिस्तर आदि की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्म रक्षा के लिए वस्त्र, छाता, शस्त्र आदि संग्रह करने पड़ते हैं। काम क्रीड़ा के लिए जोड़ीदार ढूंढ़ना पड़ता है और फिर सृष्टि संचालन के लिए सन्तान प्रेम की प्रेरणा से अन्य काम करने पड़ते हैं। इन्द्रिय रसनाएं भी शारीरिक इच्छा आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं। काया की ऐसी ही आवश्यकताओं के अनुरूप मस्तिष्क की उधेड़ बुन चलती रहती है।
अचेतन मन शरीर को जीवित रखने के लिए निरन्तर चलने वाले क्रिया-कलापों का संचालन करता है। सोते जागते जो कार्य अनवरत रूप से होने आवश्यक हैं उन्हें संभालना उसी के द्वारा होता है। रक्त संचार, श्वास-प्रश्वांस, हृदय की धड़कन, आकुंचन-प्रकुंचन, पाचन-विसर्जन आदि अनेक कार्य अचेतन मस्तिष्क अपने आप करता कराता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता। जागते में पलक झपकने की और सोते में करवट बदलने की क्रिया सहज ही होती रहती है। मस्तिष्क सम्बन्धी मोटी जानकारी इतनी ही है। प्रिय प्राप्ति पर हर्ष—अप्रिय प्रसंगों पर विषाद, भय, क्रोध, प्रेम प्रसंग छल, संघर्ष जैसी मानसिक क्रियाओं को भी सामाजिक एवं चेतनात्मक आधार पर विकसित माना जाता रहा है पर भूल उसके भी शरीर पर पड़ने वाले वर्तमान एवं भावी प्रभाव को ही समझा गया है। शरीर शास्त्रियों की दृष्टि में मस्तिष्क भी—शरीर में—शारीरिक प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला एक अवयव ही है। मुंह में ग्रास जाने की सहज प्रक्रिया के अनुसार रस-ग्रन्थियों से स्राव आरम्भ हो जाता है। दांत, जीभ आदि अपना काम सहज प्रेरणा से ही आरम्भ कर देते हैं। उसी प्रकार समझा जाता रहा है कि शरीर से सम्बद्ध समस्याओं को हल करने का उपाय ढूंढ़ने और उसकी व्यवस्था बनाने का कार्य मस्तिष्क करता है। विभिन्न अवयवों पर उसका नियन्त्रण है; तो पर क्यों है? किस प्रयोजन के लिए है? उसका उत्तर यही दिया जाता रहा है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मस्तिष्क का अस्तित्व है।
पर भावनात्मक प्रसंगों का जब सिलसिला आरम्भ होता है और उनका इतना अधिक होता है कि शारीरिक और मानसिक समस्त चेष्टाएं उसी पर केन्द्रित हो जायें यहां तक कि शरीर जैसे प्रियपात्र को त्यागने में भी संकोच न हो, तब उस भाव प्रवाह का विश्लेषण करना कठिन क्यों हो जाता है। जब हर चिन्तन और प्रयत्न शरीर की सुविधा के लिए ही नियोजित होना चाहिए तो फिर उन भावों का अस्तित्व कहां से आ गया जिनका शारीरिक लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं है। वरन् और उलटी ही हानि होती है। तब मस्तिष्क शारीरिक लाभ को, अपनी मर्यादा को छोड़कर हानि की सम्भावनाओं का समर्थन क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर दें सकना भौतिक मनःशास्त्र के लिए अभी भी सम्भव नहीं हो सका है।
दूसरों को दुखी देखकर दया क्यों आती है? किसी की सेवा करने के लिए रात भर जागने को तैयार क्यों हो जाते हैं? अपने सुविधा-साधनों का दान पुण्य क्यों किया जाता है? प्रेम पात्र के मिलने पर उल्लास और वियोग में वेदना क्यों होती है? समाज, देश, विश्व की समस्याएं क्यों प्रभावित करती हैं? धर्म रक्षा के लिए त्याग बलिदान का साहस क्यों होता है व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य, तप, तितीक्षा, जैसे कष्ट कर आचरण अपनाने के लिए उत्साह और सन्तोष क्यों होता है? भक्ति भावना में आनन्द की क्या बात है? इस प्रकार के भावनात्मक प्रयोजन जिनके साथ शारीरिक आवश्यकता एवं अभाव की पूर्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है, मनुष्य द्वारा क्यों अंगीकार किये जाते हैं और मस्तिष्क उनकी पूर्ति के लिए क्यों क्रियाशील हो उठता है?
भावनाएं क्रियाशीलता उत्पन्न करती हों सो ही नहीं वरन् कई बार वे इतनी प्रबल होती हैं कि आंधी-तूफान की तरह शरीर और मन की सामान्य क्रिया को ही अस्त-व्यस्त कर देती है। किसी प्रिय पात्र की मृत्यु का इतना आघात लग सकता है कि हृदय की गति ही रुक जाय या मस्तिष्क विकृत हो जाय। किसी नृशंस कृत्य को देखकर भयभीत मनुष्य मूर्छित हो सकता है। आत्म हत्या करने वालों की संख्या कम नहीं और वे भावोत्तेजना में ही वैसा करते हैं। ये भावनाएं मात्र शारीरिक आवश्यकता को लेकर ही नहीं उभरी होतीं।
चिन्ता, भय, शोक, क्रोध, निराशा आदि आवेशों के द्वारा होने वाली निषेधात्मक हानियों से सभी परिचित हैं वे शारीरिक रोगों से भी भयावह सिद्ध होती हैं। चिन्ता को चिता से बढ़कर बताया जाता है और कहा जाता है कि चिता मरने पर जलाती है किन्तु चिन्ता जीवित को ही जला कर रख देती है। यह भावना निषेधात्मक दिशा में गतिशील होने पर क्यों संकट उत्पन्न करती हैं और विधेयात्मक मार्ग पर चल कर क्यों अद्भुत परिणाम प्रस्तुत करती है। हमारा शरीर और मस्तिष्क क्यों उन्हें स्वीकार करता है जबकि प्रत्यक्षतः शरीर की आवश्यकताओं या सुविधाओं का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।
इस प्रश्न का उत्तर खोजते विज्ञान ने अब मस्तिष्क का भाव चेतना केन्द्र तलाश किया है। उसकी स्वल्प जानकारी अभी इतनी मिली है कि मस्तिष्क के भीतर जो मोटी और लम्बाई में फैली हुई अन्तस्त्वचा हैं उसकी तन्त्रिकाएं अपने में कुछ ऐसे रहस्य छिपाये बैठी हैं जो कारणवश भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं अथवा उनसे प्रभावित होकर उद्दीप्त होती हैं। इस संस्थान को ‘भावनात्मक मस्तिष्क’ नाम दिया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था के डा0 पाल मैकलीन, येल विश्व विद्यालय के डा0 जोसे डैलगेडी प्रभृति वैज्ञानिकों ने मनःशास्त्र के गहन विश्लेषण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रखरता की कुंजी इस भावनात्मक मस्तिष्क में ही केन्द्रीभूत है। आहार-विहार का अपना महत्व है पर उतनी व्यवस्था ठीक रखने पर भी यह निश्चित नहीं कि स्वास्थ्य ठीक ही बना रहेगा। इसी प्रकार शिक्षा एवं संगति का मस्तिष्कीय विकास से सम्बन्ध अवश्य है पर यह निश्चित नहीं कि वैसी सुविधायें मिलने पर कोई व्यक्ति मनोविकारों से रहित और स्वस्थ मस्तिष्क सम्पन्न होगा ही। उन्होंने भावनाओं का महत्व सर्वोपरि माना है और कहा है सद्भाव सम्पन्न मनुष्य शारीरिक सुविधाएं और मानसिक अनुकूलताएं न होने पर भी समग्र रूप से स्वस्थ हो सकता है। मनोविकारों से छुटकारा पाने से दीर्घजीवी बन सकता है और रोग मुक्त रह सकता है।
कहना न होगा कि स्वास्थ्य को नष्ट करने में मनोविकारों का हाथ—विषाणुओं से भी अधिक है। साथ ही समग्र स्वास्थ्य के सम्पादन में भावात्मक उत्कृष्टता का असाधारण योगदान है। अस्तु—भावात्मक मस्तिष्क की गरिमा मानवीय सत्ता में सर्वोपरि सिद्ध होती है। अध्यात्म विज्ञान इसी को अमृत घट मानता है और उसी के परिष्कार अभिवर्धन की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है।
मनःशास्त्रवेत्ता बताते हैं कि स्वस्थ और निखरे हुए मन की सभी भावात्मक अभिव्यक्तियां मुक्त रूप से होती हैं। बच्चा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्मुक्त हास्य और उन्मुक्त रुदन, दोनों ही उसमें स्पष्ट देखे जा सकते हैं।
मनुष्य को भावनात्मक संवेग प्रभावित करते ही हैं। जीवन-प्रभाव का उतार-चढ़ाव मन को भी स्पन्दित करता है। परमहंस स्थिति की बात भिन्न है। अन्यथा मनुष्य मात्र को भावनात्मक उद्वेलनों से गुजरना पड़ता है।
कौन-सी परिस्थितियां एक व्यक्ति को अनुकूल प्रतीत होती हैं, कौन प्रतिकूल? इसमें तो भिन्नता होती है। किन्तु अनुकूल परिस्थितियों से प्रसन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशानी का अनुभव स्वाभाविक है। प्रसन्नता की या आनन्द की अनुभूतियों को हंसी या मुस्कान के साथ अभिव्यक्त कर देने पर वे औरों में भी सहचरी भाव संचालित करती हैं और स्वयं का मन भी हलका हो जाता है। यदि हर्ष को गुमसुम रहकर भीतर ही दबा दिया जाय, तो भावनात्मक कोमलता को इससे क्षति पहुंचती है यही बात रोने, उदास होने के सम्बन्ध में है। मन ही मन घुटते रहने से उदासी अनेक प्रकार की ग्रन्थियों का कारण बनती है। रोने पर चित्त हलका हो जाता है, पर-दुःख कातरता उत्कृष्ट मनःस्थिति की प्रतिक्रिया है। भीतर की करुणा व संवेदना दुःख, पीड़ा और पतन के दृश्यों से तीव्रता से आंदोलित हो उठती है। यह हलचल आवश्यक है। जहां यह हलचल दबा दी जाती है। वहां इन कोमल संवेदनाओं को आघात पहुंचता है और मन की ग्रन्थियां जटिल होती जाती हैं। असफलता, असन्तोष, आघात किसके जीवन में नहीं आते। उनका आना-जाना यदि खिलाड़ी की भावना से देख ग्रहण किया जाय, तब तो चित्तभूमि के अधिक उद्वेलन का कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसी प्रशान्त मनःस्थिति तो परिष्कृत व्यक्तित्व का चिन्ह है। पर इस प्रशान्त मनोदशा में उल्लास भरपूर होता है। इसलिए अपने यहां प्रसन्न गम्भीर मनःस्थिति को सर्वोत्कृष्ट कहा—माना गया है। पर जब स्थिति ऐसी न हो मनःक्षेत्र घटनाओं को ही गुन-धुन रहा हो, तो उपयुक्त यही है कि भीतर से उठ रही रुलाई को रोका न जाय, नकली बहादुरी के प्रदर्शन का प्रयत्न मन के भीतर की घुटन को तो हल्का करेगा नहीं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को अवश्य क्षति पहुंचाएगा। भारी सदमे के कारण घातक रोग उत्पन्न होते देखे गये हैं। कई बार तो उनके कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। यदि फूट-फूट कर रो लिया गया हो याकि अपना दुःख खोलकर किसी विश्वस्त आत्मीय से विस्तारपूर्वक कह दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती।
संवेदनशील लोगों में चारों ओर के पीड़ा और पतन को देखकर मन में ‘‘मन्यु’’, सहः सहानुभूति, करुणा और संकल्प का वेग फूट पड़ता है। आत्मानुशासित संवेग सक्रिय होकर श्रेष्ठ कर्म का आधार बनता है। काव्य, चित्रकला, संगीत आदि मन का इन्हीं कोमल सम्वेदनाओं की ही तो अभिव्यक्तियां हैं। समाज-निर्माण और लोकमंगल का संकल्प ऐसी ही अनुभूतियों से दृढ़ और प्रखर होता चलता है। चारों ओर बिखरा सहज उल्लास और विराट् सौन्दर्य भी इसी प्रकार मन को अभिभूत कर उसमें ऐसी तीव्र हिलोरें उत्पन्न कर देता है कि उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती रहती है।
हंसी या आंसुओं का रासायनिक स्वरूप क्या होता है, यह महत्वहीन है। यद्यपि वे भी एक−से नहीं होते। प्रो0 स्टुटगार्ट ने भिन्न-भिन्न भावनाओं से निकल पड़ने वाले आंसुओं का अलग-अलग विश्लेषण कर यह जानकारी एकत्र की है कि इनमें से प्रत्येक प्रकार के आंसुओं में प्रोटीन, शर्करा, लवण और कीटाणुनाशक तत्वों आदि का अनुपात भिन्न-भिन्न था। साथ ही कुछ अन्य रासायनिक सम्मिश्रण भी पाये गये। इसके आधार पर उनका दावा है कि किसी व्यक्ति के अश्रुकणों के विश्लेषण द्वारा उसके रोगों का कारण बिना उस व्यक्ति से पूछे ही बताया जा सकता है।
हठात्, रुलाई रोकने से जुकाम; सिर दर्द ही नहीं, चक्कर आना, अनिद्रा, आंखें जलना, स्मरणशक्ति की कमी आदि रोग हो जाते हैं। अमरीकी मनोवैज्ञानिक जेम्सवाट के अनुसार स्त्रियां अपने आंसू बहाने में कंजूसी नहीं करने के कारण ही घुटन से मुक्त रहती हैं और अधिक स्वस्थ एवं दीर्घजीवी रहती हैं, जबकि पुरुष अपनी कठोर प्रकृति का दण्ड स्वास्थ्य के क्षरण के रूप में भोगते हैं। मनःचिकित्सक बेनार्ड होल्स ने तो अपने अर्धविक्षिप्त रोगियों को कारुणिक दृश्यों द्वारा रुलाकर उनके चित्त को हलका करते हुए उन्हें रोगमुक्त ही कर दिया।
समुद्र में ज्वार-भाटे की तरह हमारे चित्त तल में परिस्थितियों के घात-प्रतिघात हर्ष-विषाद, उल्लास-शोक के उतार-चढ़ावों की सृष्टि करते रहते हैं। उनकी सहज, मुक्त रूप में अभिव्यक्त हो जाने देना चाहिए और स्वयं बालकोचित सरलता बनाये रखना चाहिए। अधिक उत्कृष्ट स्थिति तो यही है कि मनोभूमि प्रशान्त उदार हो और द्वंद्वात्मक उभारों को सन्तुलित ही रखा जाय। पर यह स्थिति एक दिन में नहीं बन पाती। जब भीतर वैसी उदात्त मनोदशा नहीं है, तब ऊपर से भावोद्वेगों को दबा कर शान्ति बनाये रखना हानिकर ही सिद्ध होगा।
अपने दुष्कर्मों को दबाकर ऊपर से कृत्रिम शान्ति बनाये रखना, तो इन सबसे हट कर एक भिन्न ही प्रवृत्ति है। वह तो अपने सर्वनाश का ही मार्ग है। अपराधी कितना भी वीर और साहसी हो, धीरे-धीरे उसके इन गुणों का श्रेष्ठ प्रभाव घटता जाता है। दमित मनोभावनाएं गहरे मानसिक सन्ताप और जटिल रोग का कारण बनती हैं। हिटलर युवावस्था में धीर-वीर और साहसी था। पर जब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह क्रूर कर्मों की राह पर चल पड़ा, तो उसका मानसिक संताप उसे खाने लगा और खाता ही गया। उसे इसी मनस्ताप के कारण अन्तिम दिनों एक प्रकार का लकवा मार गया और उसे अपने विश्वस्तों पर भी सन्देह होने लगा।
पापकर्मों से उत्पन्न मानसिक सन्ताप तो पश्चाताप प्रक्रिया एवं आत्मस्वीकृति द्वारा ही दूर होता है। भारतीय आचार्यों ने इसी हेतु प्रायश्चित-विधान किया था और चान्द्रायण आदि व्रत कराते समय समस्त पाप स्वीकार करने होते थे।
पश्चात्ताप, पापस्वीकार और प्रायश्चित के इस विधान को कई धर्मों ने अपनाया है। अब विज्ञान भी रोगों की जड़ शरीर में नहीं मन में मानते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि हमारी अधिकांश बीमारियों का कारण पूर्वकृत पापकर्म अथवा मन में ही दबी छुपी प्रवृत्तियां दुष्प्रवृत्तियां हैं।
भावना क्षोभ से मुक्ति के लिए प्रायश्चित
घटना अमेरिका के न्यूजर्सी शाही की है। वहां के डा. नारमन वीसेण्ट पीले एक चिकित्सक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। इसके साथ ही वे न्यूजर्सी के एक चर्च में प्रवचन के लिए भी जाया करते थे। एक दिन वे प्रवचन समाप्त कर खर्च की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि एक बेचैन युवती उनके पास आ गयी और खड़ी होकर कहने लगी—‘‘डॉक्टर! क्या मेरे रोग का इस संसार में कोई इलाज ही नहीं है?’’
प्रश्न, इतनी हड़बड़ाहट में किया गया था कि एक बारगी तो डा0 पीले भी चौंक उठे। फिर उन्होंने पूछा—ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें।
युवती ने कहा कि जब भी वह चर्च में आती है तो उसकी बांहों में बड़ी तेज खुजली से वह बेहाल हो जाती है। उसने अपनी बांहों को उघाड़ कर बताया, उन पर लाल-लाल चकत्ते उभरे हुए थे। उस युवती ने यह भी कहा कि—‘‘यही हालत रही तो वह चर्च में आना बन्द कर देगी।’’
डा0 पीले ने कहा—हो सकता है तुम जिस कुर्सी पर बैठती हो उसमें कोई रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किये गये हों जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल न पड़ते हों। अगर यही बात है तो मैं जब किसी दूसरे गिरजे में जाती हूं अथवा दूसरी कुर्सी पर बैठती हूं तब तो खुजली नहीं होनी चाहिये न। लेकिन तब भी ऐसा ही होता है—युवती ने अपनी समस्या का विश्लेषण किया।
डा0 पीले एक सहृदय और प्रत्येक रोगी के प्रति सहानुभूति रखने वाले चिकित्सक थे। उन्होंने युवती को यह आश्वासन बंधाते हुए कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, कहा—‘मैं तुम्हारे फैमिली डॉक्टर से बातचीत करूंगा। शायद उनसे बातचीत के दौरान ऐसा कोई सूत्र निकल आये जिससे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके।’
युवती के फैमिली डॉक्टर का पता लेकर डा0 पीले ने उनसे सम्पर्क किया तो पता चला कि उस युवती को इन्टरनल एक्जिमा था, यह खुजली किसी रोगाणु के संक्रमण से नहीं वरन् अपने आप से भीतर ही भीतर उलझते रहने के कारण उठती है प्रायः देखा जाता है कि जब कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या बहुत कोशिश करने पर भी कोई चीज याद नहीं आ रही हो तो हाथ अपने आप उठकर कनपटियों को खुजलाने लगते हैं जब रुपये पैसों की बेहद तंगी हो और उनकी सख्त आवश्यकता अनुभव हो रही हो तो हथेलियां खुजलाने लगती हैं। यह खुजलाहट दिमाग में होने वाली उथल-पुथल के परिणामस्वरूप ही उठती हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी द्वन्द्व या संघर्ष से गुजर रहा हो तो भी जोरों की खुजली मचती है और व्यक्ति खुजाते-खुजाते चमड़ी को लाल कर लेता है। इस तरह की खुजलाहट के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर इन्टरनल एक्जिमा को पहचानते हैं।
गिरजे में आकर ही उस युवती को इस तरह की खुजली क्यों परेशान करती है—यह जानने के लिए डा0 पीले ने रोगिणी को कुरेदा। आत्मीयता, स्नेह और सहानुभूति से प्रभावित होकर उक्त युवती ने अपना सारा अतीत खोलकर रख दिया। वह किसी बड़ी फर्म में एकाउंटेन्ट के पद पर कार्य करती थी और प्रायः गोलमाल कर थोड़ा धन चुराती रहती थी। उसी युवती के अनुसार चोरी की शुरुआत बहुत छोटी रकम से की गयी थी और हर बार वह यह सोचकर पैसे चुराती थी कि वह जल्द ही इन चुराये गये पैसों को वापस रख देगी परन्तु वह ऐसा नहीं कर पायी थी।
डा. पीले ने इस घटना का विश्लेषण करते हुए कहा है कि—इस प्रकार उस युवती के मन में अपराध भावना घर कर गयी। जब वह चर्च में आती तो वहां के पवित्र वातावरण में यह भावना और उग्र हो उठती थी। परिणाम स्वरूप उसकी रक्त वाहनी की पेशियों से ऐंठन होने लगती और खुजली शुरू हो जाती।
मनःसंस्थान में जमी हुई इस रोग की जड़ों को पहचान कर डा0 पीले ने उक्त युवती को सलाह दी कि वह फर्म के मालिक के सामने सब कुछ स्वीकार कर ले साथ ही चुरायी गयी रकम को अदा करना भी शुरू कर दें। युवती ने नौकरी छूटने का डर बताया तो डा0 पीले ने ढाढ़स बंधाया हो सकता है तुम्हारी फर्म का मालिक तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर तुम्हें नौकरी से न हटाये, पर एक क्षण को यह मान भी लें कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया तो तुम्हें अन्यत्र भी नौकरी मिल सकती है। नौकरी खो देने से उतनी क्षति नहीं होगी जितनी की अपनी आत्मा और आदर्श को खोने से हो रही है।
बात समझ में आ गयी और युवती ने अपने मालिक के पास जाकर सब कुछ कह दिया। वही हुआ जिसकी सुखद सम्भावना डा. पीले ने बतायी थी। अर्थात् मालिक ने उसकी सच्चाई, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के प्रति उदित हुई दृढ़ निष्ठा से प्रभावित होकर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इस क्षमा से युवती का हृदय और पश्चाताप विदग्ध हुआ तथा उसने स्वयं ही वह पद छोड़ दिया। इस पश्चात्ताप और प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप आयी भावनाओं में शुद्धि के कारण युवती को दुबारा फिर कभी खुजली नहीं उठी। इसका कारण यह था, कि उसका भावना-जन्य क्षोभ समाप्त हो चुका था। शरीर की तमाम पेशियां स्नायु मण्डल द्वारा संचलित होती हैं। छोटी मोटी स्नायुओं का एक पूरा जाल मनुष्य शरीर में फैल हुआ है जिसका नियन्त्रण मस्तिष्क से होता है। कुछ स्नायु ऐच्छिक होते हैं, जिनका इच्छानुसार उपयोग होता है जैसे चलना-फिरना या कोई वस्तु पकड़ना छोड़ना। यह कार्य यद्यपि पेशियों द्वारा ही होते हैं, परन्तु पेशियां स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क से ही निर्देश प्राप्त करती हैं। इन ऐच्छिक स्नायुओं के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के स्नायु भी होते हैं जिन्हें अनैच्छिक कहा जाता है। इन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता और ये हृदय के धड़कने, नाड़ियों के फड़कने तथा आंतों के कांपने जैसा कार्य सम्पन्न करते हैं।
इन अनैच्छिक स्नायुओं का नियन्त्रण मस्तिष्क के उस केन्द्र से होता है जिसे ‘हायपोथैल्मस’ कहते हैं। इसी केन्द्र से एक नलिका विहीन ग्रन्थि भी सम्बन्धित रहती है जिसे पिट्यूटरी ग्रन्थि शरीर रक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसिक सन्तुलन को बनाये रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करती है। पिट्यूटरी ग्रन्थि का आकार यद्यपि एक चने के दाने के बराबर होता है परन्तु यह अन्य नलिका विहीन ग्रन्थियों का भी नियन्त्रण करती है। डा0 पीले ने जिसे युवती का मानसोपचार कर ‘इन्टरनल एक्जिमा’ ठीक किया था वह स्नायुजन्य विकास के कारण ही उत्पन्न हुआ था और भावना-क्षोभ समाप्त होते ही स्वतः ही ठीक भी हो गया।
शरीर के स्वास्थ्य संरक्षण का दायित्व पिट्यूटरी ग्रन्थि ही मुख्य रूप से सम्हालती है डा. एच. सैले ने अपनी शोधों द्वारा यह पता लगाया। यह ग्रन्थि खास तौर से उस समय ज्यादा कमजोर हो जाती है जब व्यक्ति के भीतर भावनात्मक द्वन्द्व, मानसिक उथल पुथल मची हुई हो और ऐसी स्थिति में पेशियों की ऐंठन से लेकर त्वचा विकार, हृदय रोग, पाचन विकार, रक्तचाप से लेकर हमेशा बना रहने वाला सिर दर्द तक पैदा हो सकता है। यह तो सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का संचालन मस्तिष्क द्वारा भेजे गये निर्देशों से ही होता है। भावनाओं के कारण मस्तिष्क पर अवांछनीय दबाव बना रहेगा तो यह निश्चित ही है कि उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी हो। अधिकांश रोगों के मूल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भावना क्षोभ ही पाया गया है, भले वह कोई दुराव छिपाव का भाव हो अथवा आक्रोश क्रोध का भाव।
आत्म-हत्या के मोटे एवं प्रत्यक्ष कारणों में गृहकलह, मानहानि, पश्चाताप, परीक्षा आदि प्रयोजनों में असफलता, भविष्य की निराशा, दरिद्रता, असाध्य रोग, दण्ड भय, असफल प्रेम, आदर्शवादी दुस्साहस आदि कारण गिनाये जा सकते हैं। किन्तु उसका वास्तविक कारण एक ही है मनःक्षेत्र की ऐसी दुर्बलता जो विपरीत परिस्थितियों का तनिक-सा दौर आते ही भड़क उठती है और बेकाबू होकर अनर्थ के गर्त में जा गिरती है। दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति भी तनिक-सी ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। तनिक-सी सर्दी-गर्मी न सह सकने के कारण भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को धीरे-धीरे बिगाड़ते हुए लोग उस स्थिति तक जा पहुंचते हैं जहां आत्म हत्या दुर्घटना को अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता।
चिन्तन की सही पद्धति यदि समझी और समझाई गई होती तो स्थिति को सहन या सुधारने की अभीष्ट विधि-व्यवस्था अपनाने की आदत डाली गई होती और इन आत्म-हत्या करने वालों में से अधिकांश के प्राण बच सकते थे क्योंकि वस्तुतः जीवन सम्पदा को कूड़े-करकट के ढेर में फेंक देने को विवश करने वाली कोई भी विपत्ति इस संसार में है ही नहीं।
‘मैलन कोलिय’ के रोग विषादग्रस्त रहते हैं वे दुखी, असन्तुष्ट एवं क्षुब्ध रहने के लिए कोई न कोई कारण अपने इर्द-गिर्द ही ढूंढ़ लेते हैं। किसी न किसी को अपने दुःखद चिन्तन का पात्र चुन लेते हैं। वस्तुतः वे व्यक्ति या वे परिस्थिति विक्षोभ कारक उतने नहीं होते जितना कि उन्हें गढ़ लिया है।
‘रैप्टस मेनेकलिक्स’ उस सनक का नाम है जिनमें मनुष्य दण्ड देने के लिए आतुर रहता है, पर वह इसके लिए अपने आपको ही चुनता है। आत्म-प्रताड़ना के लिए इसकी इच्छा निरन्तर उठती है। भोजन न करने, कपड़े न पहनने सिर धुनने से लेकर आत्म-हत्या करने तक की चेष्टाएं वह करता है। कभी-कभी अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तक को तोड़-फोड़कर फेंक देता है। ऐसा करने से उसे अपने विक्षोभ का समाधान होने की बात सूझती है।
दूसरों के क्षोभ को शान्त करने के लिए स्वयं दुःखी होने की स्थिति अपना लेना भी ऐसा ही विचित्र चिन्तन है जिसे अक्सर सहानुभूति एवं सहायता के लिए अपनाया जाता है। किसी स्वजन के कष्ट निवारण के लिए अपने आप की बलि किसी देवी-देवता पर चढ़ा देना अथवा विवाह योग्य कन्याओं का इसलिए आत्मघात कर बैठना कि इससे उनके अभिभावकों को अर्थचिंतन से छुटकारा मिल जायगा—ऐसे ही दुस्साहस भरे कदम हैं। इनमें आदर्शवाद, उदारता, सहानुभूति जैसे तत्वों का पुट तो होता है, पर यह स्मरण नहीं रहता कि इस कदम से अपना बहुमूल्य जीवन ही नष्ट नहीं होगा वरन् जिनके लिए यह सब किया जा रहा है उनकी कठिनाई, चिन्ता एवं विपत्ति और अधिक बढ़ जायगी।
प्राचीनकाल में आत्मघात को धार्मिक प्रशंसा प्रदान करने का भी कभी-कभी प्रचलन रहा है। इसके पीछे भारत की मूल संस्कृति नहीं वरन् सामयिक विचार विकृति ही झांकती है। संन्यासियों की स्वाभाविक मृत्यु की अपेक्षा स्वेच्छा मरण की प्रशंसा की गई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसे विधान भिक्षुजनों के लिए उनके धर्म-ग्रन्थों में मिलते हैं, भले ही वे पीछे जोड़े गये हैं। पाण्डवों का स्वर्गारोहण, मंडन मिश्र का तुषाग्नि संदाह, ज्ञानेश्वर की जीवित समाधि आदि अनेक ऐसी घटनाएं इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं, जिन्हें सराहा ही जाता है। चित्तौड़ की रानियों का सामूहिक रूप से आत्मदाह और मृत पतियों के साथ अनेक पत्नियों का सती हो जाना ऐसे ही कृत्यों में गिना जाता है जिसके लिए उन्हें प्रशंसा योग्य ठहराया जाय।
इतिहास पुराणों में ऐसे अनेकों घटना प्रसंग उपलब्ध हैं जिनमें कतिपय नर-नारियों ने धार्मिक प्रयोजनों के लिए अथवा दूसरों की तुलना में अपने को अधिक आदर्शवादी, अधिक साहसी सिद्ध करने के लिए आत्मघात किये हैं। पराजित एवं असफल लोगों द्वारा प्राण त्याग करके अपनी ग्लानि मिटाने की घटनाएं तो सदा ही होती रही हैं। उन्हें लोगों ने सराहा तो नहीं, पर सहानुभूति की दृष्टि से अवश्य देखा। मृतकों के लिए यह सहानुभूति चिन्तन भी प्रेरक बना। आत्मघात का साहस न कर सकने पर अपनी सन्तान की अथवा पशु-पक्षियों की बलि चढ़ा देने की प्रथा तो एक प्रकार से किसी काल में मान्यता प्राप्त धर्म कृत्य बन गई थी और कहीं-कहीं अभी तक उसका प्रचलन मौजूद है।
आत्म-हत्या को भी दूसरों की हत्या के समान ही गर्हित कर्म माना जा सकता है। प्राचीनकाल में इसे बहुत बुरा कहा जाता था और मरने के उपरान्त भी इस कुकृत्य करने वाले की भर्त्सना की जाती थी।
योरोप में उन दिनों आत्म-हत्या करने वालों के प्रति बहुत अनुदार दृष्टिकोण था। उनकी लाशें सड़कों के आस-पास कूड़े के ढेर में दबादी जाती थीं और भयंकर आकृतियां वहां खड़ी कर दी जाती थीं, ताकि उन मरने वालों की बदनामी हो। इन परिस्थितियों को बदलने में डेविडह्यूम, वाल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने आवाज उठाई थी और कहा था, आदमी को जीने की तरह मरने की भी आजादी होनी चाहिए।
कुरान में दूसरों की हत्या करने से भी अधिक जघन्य पाप आत्म-हत्या को बताया है। यहूदी धर्म में भी ऐसा ही है, उसमें आत्म-हत्या करने वाले के लिए शोक मनाने और उसकी आत्मा को शान्ति देने के लिए प्रार्थना करने की भी मनाही है। ईसाई धर्म में भी इसे घृणित पातक बताया गया है। 11 वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में एक कानून बना था, जिसमें आत्म-हत्या करने वाले की सम्पत्ति जब्त करली जाती थी और उसके शव को किसी ईसाई कब्रिस्तान में धार्मिक विधि से दफनाया नहीं जा सकता था।
आत्म-हत्या का प्रयत्न करने वाले को रोगी माना जाय या अपराधी? इस प्रश्न के उत्तर में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे लोगों का उचित स्थान जेलखाना नहीं, वरन् पागलखाना है। भारत सरकार की मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति को तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा0 सुशीला नैयर ने सुझाव दिया था कि आत्महत्या की चेष्टा एक मानसिक विकृति है इसलिए इस प्रकार का प्रयत्न करने वालों को अपराधी नहीं वरन् रुग्ण व्यक्ति माना जाना चाहिए। अब इंग्लैण्ड के कानूनों में भी इस सन्दर्भ में सुधार कर लिया गया है उन्हें दण्डनीय नहीं माना जाता।
पागलपन भी मानसिक दुर्बलता के कारण उत्पन्न होने वाली मनोव्याधि है। अब तक इस रोग का विद्युतीय उपचार किया जाता है पर पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने इन रोगों का अन्य उपायों से उपचार करने की विधि भी खोज निकाली है।
मनोरोगों का प्रेमोपचार
विश्व विख्यात मनःशास्त्री टामस मैलोन ने पागलपन के कारण ढूंढ़ने वाले अनेकों शोध संस्थानों का मार्गदर्शन किया है और उन्हें परीक्षणों के आधार पर किसी उपयुक्त निष्कर्षों तक पहुंचाने में सहायता की है। उनके अनुसन्धानों के निष्कर्षों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह पाया है कि ‘मनुष्य दूसरों का प्यार पाना चाहता है; पर वह उसे मिल नहीं पाता। इस अभाव से उसके अन्तःक्षेत्र की गहरी परतों में निराशा जन्य उदासी छा जाती है। फलतः उसका चिन्तन प्रवाह अपना सीधा रास्ता छोड़कर भटकावों में फंस जाता है। प्यार पाने की असफलता का कारण सम्भव है उस व्यक्ति के अपने ही दोष दुर्गुणों में रहा हो, पर इससे क्या, उसकी आकांक्षा तो अतृप्त ही रह गई। वह यह समीक्षा कहां कर पाता है कि दोष अपना है या पराया। भोजन किसी भी कारण न मिले, पेट का विक्षोभ तो हर हालत में रहेगा ही। इसी प्रकार प्यार के अभाव में मनुष्य अपना मानसिक सन्तुलन धीरे-धीरे खोता चला जाता है और एक दिन स्थिति वह आ जाती है जिसमें उसे विक्षिप्त एवं अर्द्ध-विक्षिप्त के रूप में पाया जाता है।
जो पूर्ण विक्षिप्त हो चुके हैं उनकी बात दूसरी है, पर जो दूसरों के मन और व्यवहार का अन्तर समझने में किसी सीमा तक समर्थ हैं उनके रोग को साध्य माना जा सकता है। अधिक से अधिक यह समझा जा सकता है कि उपचार कष्ट साध्य है, पर असाध्य तो नहीं ही कहना चाहिए। ऐसे रोगियों का उपयुक्त उपचार यह है कि उन्हें उपेक्षा के वातावरण से निकाल कर स्नेह-सद्भाव का अनुभव करने दिया जाय। जिनसे उसका वास्ता पड़ता है वे सभी उसे प्यार और सम्मान प्रदान करें। वैसा न करें जैसा कि आमतौर से पागलों के साथ किया जाता है। अटपटेपन पर खीज आना स्वाभाविक है, पर हितैषियों को यह मानकर चलना चाहिए कि रोगी आखिर रोगी है और उसके अटपटे व्यवहार जान-बूझकर की गई उद्धतता नहीं वरन् चिन्तन तन्त्र के गड़बड़ा जाने की विवशता भर है। ऐसी दशा में वह तिरस्कार एवं प्रताड़ना का नहीं, दया और दुलार का अधिकारी है।
प्यार की प्यास मानवी चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। पदार्थों के संग्रह इन्द्रियों की रसानुभूति के उपरान्त तीसरी भूख स्नेह की है जो व्यवहार में सम्मान के रूप में देखी जाती है। यश कामना उसी का रूप है। प्रतिष्ठा प्राप्त करते समय मनुष्य सोचता है कि यह सम्मान कर्ताओं द्वारा दिया गया स्नेह सद्भाव है। यों होता यह भ्रम ही है किन्तु असली न मिलने पर नकली से भी बहुत करके काम चलाते रहा जाता है। स्नेह के साथ सम्मान रहेगा किन्तु सम्मान का प्रदर्शन सदा स्नेह युक्त ही हो यह आवश्यक नहीं। उसमें छद्म भी घुला रह सकता है। सम्मान और यश के लिए लालायित प्रायः सभी पाये जाते हैं और उसके लिए समय, श्रम एवं धन भी खर्च करते हैं। यश लालसा के पीछे वस्तुतः प्यार को उपलब्ध करने की आकांक्षा ही काम करती है। लोग बड़प्पन के प्रदर्शन में उसे खरीदने की विडम्बना रचते रहते हैं।
पानी की प्यास से गला सूखता है और भूख से पेट उठता है। प्यार के अभाव में आदमी थकता नहीं टूटता भी है। एकाकीपन यों अन्य प्राणियों को भी सहन नहीं, पर मनुष्य के लिए तो वह ढोया जा सकने वाला भार है। वह साथ रहना ही नहीं चाहता ऐसे साथी भी चाहता है जो उसके अन्तस् को छूने, गुदगुदाने खड़ा रखने और उठाने में सहायता कर सकें। प्यार का अभाव अखरता तो धैर्यवानों को भी है, पर हलकापन तो उसके कारण उखड़ ही जाता है। प्रायः आन्तरिक उखड़ापन ही पगलाने की व्यथा बन कर सामने आती है। यों पागलपन के इसके अतिरिक्त भी और भी कितने ही कारण होते हैं।
इस प्रकार पगलाने वालों का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि वे प्यार की प्रकृति को नहीं जानते और यह नहीं समझ पाते कि यह अपने भीतर से निकलने वाली आभा भर है जो जहां भी पड़ती है वहां दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक चमक उत्पन्न करती और आकर्षक लगती है। अपना प्यार ही दूसरों में प्रतिबिंबित होता है। यदि उसमें कमी हो तो दूसरों का वास्तविक सद्भाव भी ठीक तरह समझ सकना सम्भव न हो सकेगा। इसके विपरीत अपनी प्रगाढ़ आत्मीयता होने पर साथियों का सामान्य शिष्टाचार भी गहरे दुलार की अनुभूति करता रहता है। बल्ब स्वयं जलता है और अपने क्षेत्र को प्रकाशवान करता है। व्यक्ति का अपना प्यार ही है जो विकसित होने पर दूसरों में प्रेम प्रतिदान मिलने के रूप में विदित होता रहता है।
जो इस तथ्य को समझते हैं वे पगलाने से बचे रहते हैं। चपेट में आते हैं तो अपना उपचार आप कर लेते हैं। दूसरों की प्रतीक्षा न करके अपनी ओर से सद्भाव बढ़ाते हैं और उसे साथियों में, सम्पर्क क्षेत्र में उसका प्रतिबिम्ब देखते हैं। मानसिक अवसाद का यह अति सरल किन्तु अत्यन्त कारगर स्वसंचालित उपचार है, पर दुर्भाग्य यह है कि इस तथ्य को कोई-कोई ही समझ पाते हैं। और अपनी ओर न देखकर स्नेह, सद्व्यवहार एवं सम्मान के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। न मिलने पर खीजते और दूसरों पर ही कृपणता, कृतघ्नता आदि का दोष लगाते हैं। सहयोग के अभाव में सांसारिक कामों में हानि पड़ने की बात सर्वविदित है। आन्तरिक सद्भावों की उपलब्धि भी उससे भी बड़ी आवश्यकता है। इतने बड़े उपार्जन का यही सरल उपाय है कि अपनी ओर से प्यार का प्रकाश फेंककर दूसरों को प्रिय पात्र बना लिया जाय और अपने ही प्रेम प्रकाश का आलोक समीपवर्ती क्षेत्र में छाया देखा जाय।
मानसोपचार की कठिनाई यह होती है कि वह पगलाये हुए रोगियों को यह दार्शनिक तथ्य समझा सकने में सफल नहीं हो पाते, समझने में तथाकथित समझदार भी असफल रहते हैं। मानसिक रोगी पहले तो अपनी विपन्नता ही स्वीकार नहीं करता, करता भी है तो उसे दूसरों की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई मानता है। जब तथ्य को स्वीकार ही नहीं किया गया तो उसके परिवर्तन के लिए बताया गया उपाय भी किस तरह गले उतरेगा। कदाचित ही कोई मनोरोग चिकित्सक अपने रोगियों को यह समझा सकने में सफल हो पाते होंगे कि उन्हें अपने भीतर आशा का, उल्लास का, प्रेम का स्रोत उभारना चाहिए और अपने सूखे मनःक्षेत्र को हरा-भरा कर लेना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है कि दो वयस्क मस्तिष्क लाख प्रयत्न करने पर भी उस तथ्य को समझने और समझाने में सफल नहीं होते, जिन पर कि उनकी प्रसन्नता और सफलता निर्भर है। जो हो, उपचार तो करना ही ठहरा। ऐसी दशा में एक ही उपाय शेष रह जाता है कि विक्षिप्तता एवं अर्ध विक्षिप्तता के रोगी से सहानुभूति रखने वाले सभी लोग अपना व्यवहार बदल लें। स्नेह, सहयोग और सम्मान का प्रदर्शन करें। आत्मीयजन होने के नाते यदि ऐसा सहज स्वाभाविक रूप से बन पड़े तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, पर यदि भीतर से वैसी उमंग न उठतीं हो तो भी प्रेम प्रदर्शन को कारगर उपचार मानकर उसके लिए आवश्यक प्रयास किया जाना चाहिए।
मानसोपचार में औषधियों का—विद्युत प्रयोगों का तथा अन्यान्य क्रिया-प्रक्रियाओं का भी महत्व है, पर उन सबके संयुक्त परिणाम में भी अधिक लाभदायक यह होता है कि पगलाये रोगी को स्नेह दुलार के वातावरण में रहने का अनुभव होने लगे। उद्धत मनोरोगियों की आक्रामक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने एवं सामान्य शिष्टाचार खो बैठने पर प्रतिबन्धित भी किया जाता है और वैसा करने से उसे क्या हानि उठानी पड़ेगी इसका अनुभव भी कराना चाहिए। अन्यथा उद्धत आचरण बढ़ता ही जायगा। इतने पर भी यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि मानसिक रोगों के रूप में जीवन की नाव में जो पानी घुसता है उसके प्रवेश द्वारा को प्यार के अभाव की अनुभूति ही कहा जा सकता है। अवसाद को उत्साह में बदल देना ही मानसिक रोगों की कारगर चिकित्सा है। इसमें प्रेमोपचार को जितनी सफलता मिलती है उतनी और किसी प्रयोग को नहीं। पहले कभी समझा जाता रहा था कि सोच समझ, विचार और सूझ बूझ मस्तिष्क का काम है—तथा भावनायें-संवेदनायें हृदय का। लेकिन यह धारणा कई वर्षों पहले गलत सिद्ध हो चुकी हैं और भावनाओं का क्रीड़ाक्षेत्र भी मस्तिष्क ही माना जाने लगा है। मानव मस्तिष्क के इस भाग को और अभी बहुत कम ही स्थान दिया गया है। इस भावनात्मक मस्तिष्क के खोज का कार्य अभी नितान्त आरम्भिक अवस्था में ही माना जा सकता है। मस्तिष्क के भीतर मोटी और काफी लम्बाई तक फैली हुई अन्तस्त्वचा के भीतर विशिष्ट प्रकार की तन्त्रिकाएं फैली हुई हैं। यद्यपि यह मस्तिष्क के प्रचलित वर्गीकरण में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकती हैं तो भी यह देखा जाता है कि सुख, दुख, भय, हर्ष, क्रोध, आवेश, करुणा, सेवा-स्नेह, कामुकता, उदारता, संकीर्णता, छल, प्रेम, द्वेष आदि भावनाओं का इसी स्थान से सम्बन्ध है। और ये भावनाएं ही हैं जो चेतन ही नहीं अचेतन मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। इच्छा संचालित और अनिच्छा संचालित केन्द्रों में भारी उलट पुलट प्रस्तुत करती हैं।
कुछ दिन पहले शारीरिक आवश्यकतानुसार मानसिक क्रियाकलाप की गतिविधियों का चलना माना जाता था। भूख लगती है तो पेट भरने की चिन्ता मस्तिष्क को होती है और पैर वैसी सुविधा वाले स्थान तक पहुंचते हैं जहां हाथ खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। मुंह चबाता है और पेट पचाता है। इसी प्रकार आहार के उपरान्त निद्रा, विश्राम के लिए, छाया घर निवास की—शैया, बिस्तर आदि की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्म रक्षा के लिए वस्त्र, छाता, शस्त्र आदि संग्रह करने पड़ते हैं। काम क्रीड़ा के लिए जोड़ीदार ढूंढ़ना पड़ता है और फिर सृष्टि संचालन के लिए सन्तान प्रेम की प्रेरणा से अन्य काम करने पड़ते हैं। इन्द्रिय रसनाएं भी शारीरिक इच्छा आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं। काया की ऐसी ही आवश्यकताओं के अनुरूप मस्तिष्क की उधेड़ बुन चलती रहती है।
अचेतन मन शरीर को जीवित रखने के लिए निरन्तर चलने वाले क्रिया-कलापों का संचालन करता है। सोते जागते जो कार्य अनवरत रूप से होने आवश्यक हैं उन्हें संभालना उसी के द्वारा होता है। रक्त संचार, श्वास-प्रश्वांस, हृदय की धड़कन, आकुंचन-प्रकुंचन, पाचन-विसर्जन आदि अनेक कार्य अचेतन मस्तिष्क अपने आप करता कराता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता। जागते में पलक झपकने की और सोते में करवट बदलने की क्रिया सहज ही होती रहती है। मस्तिष्क सम्बन्धी मोटी जानकारी इतनी ही है। प्रिय प्राप्ति पर हर्ष—अप्रिय प्रसंगों पर विषाद, भय, क्रोध, प्रेम प्रसंग छल, संघर्ष जैसी मानसिक क्रियाओं को भी सामाजिक एवं चेतनात्मक आधार पर विकसित माना जाता रहा है पर भूल उसके भी शरीर पर पड़ने वाले वर्तमान एवं भावी प्रभाव को ही समझा गया है। शरीर शास्त्रियों की दृष्टि में मस्तिष्क भी—शरीर में—शारीरिक प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला एक अवयव ही है। मुंह में ग्रास जाने की सहज प्रक्रिया के अनुसार रस-ग्रन्थियों से स्राव आरम्भ हो जाता है। दांत, जीभ आदि अपना काम सहज प्रेरणा से ही आरम्भ कर देते हैं। उसी प्रकार समझा जाता रहा है कि शरीर से सम्बद्ध समस्याओं को हल करने का उपाय ढूंढ़ने और उसकी व्यवस्था बनाने का कार्य मस्तिष्क करता है। विभिन्न अवयवों पर उसका नियन्त्रण है; तो पर क्यों है? किस प्रयोजन के लिए है? उसका उत्तर यही दिया जाता रहा है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मस्तिष्क का अस्तित्व है।
पर भावनात्मक प्रसंगों का जब सिलसिला आरम्भ होता है और उनका इतना अधिक होता है कि शारीरिक और मानसिक समस्त चेष्टाएं उसी पर केन्द्रित हो जायें यहां तक कि शरीर जैसे प्रियपात्र को त्यागने में भी संकोच न हो, तब उस भाव प्रवाह का विश्लेषण करना कठिन क्यों हो जाता है। जब हर चिन्तन और प्रयत्न शरीर की सुविधा के लिए ही नियोजित होना चाहिए तो फिर उन भावों का अस्तित्व कहां से आ गया जिनका शारीरिक लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं है। वरन् और उलटी ही हानि होती है। तब मस्तिष्क शारीरिक लाभ को, अपनी मर्यादा को छोड़कर हानि की सम्भावनाओं का समर्थन क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर दें सकना भौतिक मनःशास्त्र के लिए अभी भी सम्भव नहीं हो सका है।
दूसरों को दुखी देखकर दया क्यों आती है? किसी की सेवा करने के लिए रात भर जागने को तैयार क्यों हो जाते हैं? अपने सुविधा-साधनों का दान पुण्य क्यों किया जाता है? प्रेम पात्र के मिलने पर उल्लास और वियोग में वेदना क्यों होती है? समाज, देश, विश्व की समस्याएं क्यों प्रभावित करती हैं? धर्म रक्षा के लिए त्याग बलिदान का साहस क्यों होता है व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य, तप, तितीक्षा, जैसे कष्ट कर आचरण अपनाने के लिए उत्साह और सन्तोष क्यों होता है? भक्ति भावना में आनन्द की क्या बात है? इस प्रकार के भावनात्मक प्रयोजन जिनके साथ शारीरिक आवश्यकता एवं अभाव की पूर्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है, मनुष्य द्वारा क्यों अंगीकार किये जाते हैं और मस्तिष्क उनकी पूर्ति के लिए क्यों क्रियाशील हो उठता है?
भावनाएं क्रियाशीलता उत्पन्न करती हों सो ही नहीं वरन् कई बार वे इतनी प्रबल होती हैं कि आंधी-तूफान की तरह शरीर और मन की सामान्य क्रिया को ही अस्त-व्यस्त कर देती है। किसी प्रिय पात्र की मृत्यु का इतना आघात लग सकता है कि हृदय की गति ही रुक जाय या मस्तिष्क विकृत हो जाय। किसी नृशंस कृत्य को देखकर भयभीत मनुष्य मूर्छित हो सकता है। आत्म हत्या करने वालों की संख्या कम नहीं और वे भावोत्तेजना में ही वैसा करते हैं। ये भावनाएं मात्र शारीरिक आवश्यकता को लेकर ही नहीं उभरी होतीं।
चिन्ता, भय, शोक, क्रोध, निराशा आदि आवेशों के द्वारा होने वाली निषेधात्मक हानियों से सभी परिचित हैं वे शारीरिक रोगों से भी भयावह सिद्ध होती हैं। चिन्ता को चिता से बढ़कर बताया जाता है और कहा जाता है कि चिता मरने पर जलाती है किन्तु चिन्ता जीवित को ही जला कर रख देती है। यह भावना निषेधात्मक दिशा में गतिशील होने पर क्यों संकट उत्पन्न करती हैं और विधेयात्मक मार्ग पर चल कर क्यों अद्भुत परिणाम प्रस्तुत करती है। हमारा शरीर और मस्तिष्क क्यों उन्हें स्वीकार करता है जबकि प्रत्यक्षतः शरीर की आवश्यकताओं या सुविधाओं का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।
इस प्रश्न का उत्तर खोजते विज्ञान ने अब मस्तिष्क का भाव चेतना केन्द्र तलाश किया है। उसकी स्वल्प जानकारी अभी इतनी मिली है कि मस्तिष्क के भीतर जो मोटी और लम्बाई में फैली हुई अन्तस्त्वचा हैं उसकी तन्त्रिकाएं अपने में कुछ ऐसे रहस्य छिपाये बैठी हैं जो कारणवश भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं अथवा उनसे प्रभावित होकर उद्दीप्त होती हैं। इस संस्थान को ‘भावनात्मक मस्तिष्क’ नाम दिया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था के डा0 पाल मैकलीन, येल विश्व विद्यालय के डा0 जोसे डैलगेडी प्रभृति वैज्ञानिकों ने मनःशास्त्र के गहन विश्लेषण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रखरता की कुंजी इस भावनात्मक मस्तिष्क में ही केन्द्रीभूत है। आहार-विहार का अपना महत्व है पर उतनी व्यवस्था ठीक रखने पर भी यह निश्चित नहीं कि स्वास्थ्य ठीक ही बना रहेगा। इसी प्रकार शिक्षा एवं संगति का मस्तिष्कीय विकास से सम्बन्ध अवश्य है पर यह निश्चित नहीं कि वैसी सुविधायें मिलने पर कोई व्यक्ति मनोविकारों से रहित और स्वस्थ मस्तिष्क सम्पन्न होगा ही। उन्होंने भावनाओं का महत्व सर्वोपरि माना है और कहा है सद्भाव सम्पन्न मनुष्य शारीरिक सुविधाएं और मानसिक अनुकूलताएं न होने पर भी समग्र रूप से स्वस्थ हो सकता है। मनोविकारों से छुटकारा पाने से दीर्घजीवी बन सकता है और रोग मुक्त रह सकता है।
कहना न होगा कि स्वास्थ्य को नष्ट करने में मनोविकारों का हाथ—विषाणुओं से भी अधिक है। साथ ही समग्र स्वास्थ्य के सम्पादन में भावात्मक उत्कृष्टता का असाधारण योगदान है। अस्तु—भावात्मक मस्तिष्क की गरिमा मानवीय सत्ता में सर्वोपरि सिद्ध होती है। अध्यात्म विज्ञान इसी को अमृत घट मानता है और उसी के परिष्कार अभिवर्धन की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है।
मनःशास्त्रवेत्ता बताते हैं कि स्वस्थ और निखरे हुए मन की सभी भावात्मक अभिव्यक्तियां मुक्त रूप से होती हैं। बच्चा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्मुक्त हास्य और उन्मुक्त रुदन, दोनों ही उसमें स्पष्ट देखे जा सकते हैं।
मनुष्य को भावनात्मक संवेग प्रभावित करते ही हैं। जीवन-प्रभाव का उतार-चढ़ाव मन को भी स्पन्दित करता है। परमहंस स्थिति की बात भिन्न है। अन्यथा मनुष्य मात्र को भावनात्मक उद्वेलनों से गुजरना पड़ता है।
कौन-सी परिस्थितियां एक व्यक्ति को अनुकूल प्रतीत होती हैं, कौन प्रतिकूल? इसमें तो भिन्नता होती है। किन्तु अनुकूल परिस्थितियों से प्रसन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशानी का अनुभव स्वाभाविक है। प्रसन्नता की या आनन्द की अनुभूतियों को हंसी या मुस्कान के साथ अभिव्यक्त कर देने पर वे औरों में भी सहचरी भाव संचालित करती हैं और स्वयं का मन भी हलका हो जाता है। यदि हर्ष को गुमसुम रहकर भीतर ही दबा दिया जाय, तो भावनात्मक कोमलता को इससे क्षति पहुंचती है यही बात रोने, उदास होने के सम्बन्ध में है। मन ही मन घुटते रहने से उदासी अनेक प्रकार की ग्रन्थियों का कारण बनती है। रोने पर चित्त हलका हो जाता है, पर-दुःख कातरता उत्कृष्ट मनःस्थिति की प्रतिक्रिया है। भीतर की करुणा व संवेदना दुःख, पीड़ा और पतन के दृश्यों से तीव्रता से आंदोलित हो उठती है। यह हलचल आवश्यक है। जहां यह हलचल दबा दी जाती है। वहां इन कोमल संवेदनाओं को आघात पहुंचता है और मन की ग्रन्थियां जटिल होती जाती हैं। असफलता, असन्तोष, आघात किसके जीवन में नहीं आते। उनका आना-जाना यदि खिलाड़ी की भावना से देख ग्रहण किया जाय, तब तो चित्तभूमि के अधिक उद्वेलन का कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसी प्रशान्त मनःस्थिति तो परिष्कृत व्यक्तित्व का चिन्ह है। पर इस प्रशान्त मनोदशा में उल्लास भरपूर होता है। इसलिए अपने यहां प्रसन्न गम्भीर मनःस्थिति को सर्वोत्कृष्ट कहा—माना गया है। पर जब स्थिति ऐसी न हो मनःक्षेत्र घटनाओं को ही गुन-धुन रहा हो, तो उपयुक्त यही है कि भीतर से उठ रही रुलाई को रोका न जाय, नकली बहादुरी के प्रदर्शन का प्रयत्न मन के भीतर की घुटन को तो हल्का करेगा नहीं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को अवश्य क्षति पहुंचाएगा। भारी सदमे के कारण घातक रोग उत्पन्न होते देखे गये हैं। कई बार तो उनके कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। यदि फूट-फूट कर रो लिया गया हो याकि अपना दुःख खोलकर किसी विश्वस्त आत्मीय से विस्तारपूर्वक कह दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती।
संवेदनशील लोगों में चारों ओर के पीड़ा और पतन को देखकर मन में ‘‘मन्यु’’, सहः सहानुभूति, करुणा और संकल्प का वेग फूट पड़ता है। आत्मानुशासित संवेग सक्रिय होकर श्रेष्ठ कर्म का आधार बनता है। काव्य, चित्रकला, संगीत आदि मन का इन्हीं कोमल सम्वेदनाओं की ही तो अभिव्यक्तियां हैं। समाज-निर्माण और लोकमंगल का संकल्प ऐसी ही अनुभूतियों से दृढ़ और प्रखर होता चलता है। चारों ओर बिखरा सहज उल्लास और विराट् सौन्दर्य भी इसी प्रकार मन को अभिभूत कर उसमें ऐसी तीव्र हिलोरें उत्पन्न कर देता है कि उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती रहती है।
हंसी या आंसुओं का रासायनिक स्वरूप क्या होता है, यह महत्वहीन है। यद्यपि वे भी एक−से नहीं होते। प्रो0 स्टुटगार्ट ने भिन्न-भिन्न भावनाओं से निकल पड़ने वाले आंसुओं का अलग-अलग विश्लेषण कर यह जानकारी एकत्र की है कि इनमें से प्रत्येक प्रकार के आंसुओं में प्रोटीन, शर्करा, लवण और कीटाणुनाशक तत्वों आदि का अनुपात भिन्न-भिन्न था। साथ ही कुछ अन्य रासायनिक सम्मिश्रण भी पाये गये। इसके आधार पर उनका दावा है कि किसी व्यक्ति के अश्रुकणों के विश्लेषण द्वारा उसके रोगों का कारण बिना उस व्यक्ति से पूछे ही बताया जा सकता है।
हठात्, रुलाई रोकने से जुकाम; सिर दर्द ही नहीं, चक्कर आना, अनिद्रा, आंखें जलना, स्मरणशक्ति की कमी आदि रोग हो जाते हैं। अमरीकी मनोवैज्ञानिक जेम्सवाट के अनुसार स्त्रियां अपने आंसू बहाने में कंजूसी नहीं करने के कारण ही घुटन से मुक्त रहती हैं और अधिक स्वस्थ एवं दीर्घजीवी रहती हैं, जबकि पुरुष अपनी कठोर प्रकृति का दण्ड स्वास्थ्य के क्षरण के रूप में भोगते हैं। मनःचिकित्सक बेनार्ड होल्स ने तो अपने अर्धविक्षिप्त रोगियों को कारुणिक दृश्यों द्वारा रुलाकर उनके चित्त को हलका करते हुए उन्हें रोगमुक्त ही कर दिया।
समुद्र में ज्वार-भाटे की तरह हमारे चित्त तल में परिस्थितियों के घात-प्रतिघात हर्ष-विषाद, उल्लास-शोक के उतार-चढ़ावों की सृष्टि करते रहते हैं। उनकी सहज, मुक्त रूप में अभिव्यक्त हो जाने देना चाहिए और स्वयं बालकोचित सरलता बनाये रखना चाहिए। अधिक उत्कृष्ट स्थिति तो यही है कि मनोभूमि प्रशान्त उदार हो और द्वंद्वात्मक उभारों को सन्तुलित ही रखा जाय। पर यह स्थिति एक दिन में नहीं बन पाती। जब भीतर वैसी उदात्त मनोदशा नहीं है, तब ऊपर से भावोद्वेगों को दबा कर शान्ति बनाये रखना हानिकर ही सिद्ध होगा।
अपने दुष्कर्मों को दबाकर ऊपर से कृत्रिम शान्ति बनाये रखना, तो इन सबसे हट कर एक भिन्न ही प्रवृत्ति है। वह तो अपने सर्वनाश का ही मार्ग है। अपराधी कितना भी वीर और साहसी हो, धीरे-धीरे उसके इन गुणों का श्रेष्ठ प्रभाव घटता जाता है। दमित मनोभावनाएं गहरे मानसिक सन्ताप और जटिल रोग का कारण बनती हैं। हिटलर युवावस्था में धीर-वीर और साहसी था। पर जब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह क्रूर कर्मों की राह पर चल पड़ा, तो उसका मानसिक संताप उसे खाने लगा और खाता ही गया। उसे इसी मनस्ताप के कारण अन्तिम दिनों एक प्रकार का लकवा मार गया और उसे अपने विश्वस्तों पर भी सन्देह होने लगा।
पापकर्मों से उत्पन्न मानसिक सन्ताप तो पश्चाताप प्रक्रिया एवं आत्मस्वीकृति द्वारा ही दूर होता है। भारतीय आचार्यों ने इसी हेतु प्रायश्चित-विधान किया था और चान्द्रायण आदि व्रत कराते समय समस्त पाप स्वीकार करने होते थे।
पश्चात्ताप, पापस्वीकार और प्रायश्चित के इस विधान को कई धर्मों ने अपनाया है। अब विज्ञान भी रोगों की जड़ शरीर में नहीं मन में मानते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि हमारी अधिकांश बीमारियों का कारण पूर्वकृत पापकर्म अथवा मन में ही दबी छुपी प्रवृत्तियां दुष्प्रवृत्तियां हैं।
भावना क्षोभ से मुक्ति के लिए प्रायश्चित
घटना अमेरिका के न्यूजर्सी शाही की है। वहां के डा. नारमन वीसेण्ट पीले एक चिकित्सक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। इसके साथ ही वे न्यूजर्सी के एक चर्च में प्रवचन के लिए भी जाया करते थे। एक दिन वे प्रवचन समाप्त कर खर्च की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि एक बेचैन युवती उनके पास आ गयी और खड़ी होकर कहने लगी—‘‘डॉक्टर! क्या मेरे रोग का इस संसार में कोई इलाज ही नहीं है?’’
प्रश्न, इतनी हड़बड़ाहट में किया गया था कि एक बारगी तो डा0 पीले भी चौंक उठे। फिर उन्होंने पूछा—ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें।
युवती ने कहा कि जब भी वह चर्च में आती है तो उसकी बांहों में बड़ी तेज खुजली से वह बेहाल हो जाती है। उसने अपनी बांहों को उघाड़ कर बताया, उन पर लाल-लाल चकत्ते उभरे हुए थे। उस युवती ने यह भी कहा कि—‘‘यही हालत रही तो वह चर्च में आना बन्द कर देगी।’’
डा0 पीले ने कहा—हो सकता है तुम जिस कुर्सी पर बैठती हो उसमें कोई रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किये गये हों जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल न पड़ते हों। अगर यही बात है तो मैं जब किसी दूसरे गिरजे में जाती हूं अथवा दूसरी कुर्सी पर बैठती हूं तब तो खुजली नहीं होनी चाहिये न। लेकिन तब भी ऐसा ही होता है—युवती ने अपनी समस्या का विश्लेषण किया।
डा0 पीले एक सहृदय और प्रत्येक रोगी के प्रति सहानुभूति रखने वाले चिकित्सक थे। उन्होंने युवती को यह आश्वासन बंधाते हुए कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, कहा—‘मैं तुम्हारे फैमिली डॉक्टर से बातचीत करूंगा। शायद उनसे बातचीत के दौरान ऐसा कोई सूत्र निकल आये जिससे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके।’
युवती के फैमिली डॉक्टर का पता लेकर डा0 पीले ने उनसे सम्पर्क किया तो पता चला कि उस युवती को इन्टरनल एक्जिमा था, यह खुजली किसी रोगाणु के संक्रमण से नहीं वरन् अपने आप से भीतर ही भीतर उलझते रहने के कारण उठती है प्रायः देखा जाता है कि जब कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या बहुत कोशिश करने पर भी कोई चीज याद नहीं आ रही हो तो हाथ अपने आप उठकर कनपटियों को खुजलाने लगते हैं जब रुपये पैसों की बेहद तंगी हो और उनकी सख्त आवश्यकता अनुभव हो रही हो तो हथेलियां खुजलाने लगती हैं। यह खुजलाहट दिमाग में होने वाली उथल-पुथल के परिणामस्वरूप ही उठती हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी द्वन्द्व या संघर्ष से गुजर रहा हो तो भी जोरों की खुजली मचती है और व्यक्ति खुजाते-खुजाते चमड़ी को लाल कर लेता है। इस तरह की खुजलाहट के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर इन्टरनल एक्जिमा को पहचानते हैं।
गिरजे में आकर ही उस युवती को इस तरह की खुजली क्यों परेशान करती है—यह जानने के लिए डा0 पीले ने रोगिणी को कुरेदा। आत्मीयता, स्नेह और सहानुभूति से प्रभावित होकर उक्त युवती ने अपना सारा अतीत खोलकर रख दिया। वह किसी बड़ी फर्म में एकाउंटेन्ट के पद पर कार्य करती थी और प्रायः गोलमाल कर थोड़ा धन चुराती रहती थी। उसी युवती के अनुसार चोरी की शुरुआत बहुत छोटी रकम से की गयी थी और हर बार वह यह सोचकर पैसे चुराती थी कि वह जल्द ही इन चुराये गये पैसों को वापस रख देगी परन्तु वह ऐसा नहीं कर पायी थी।
डा. पीले ने इस घटना का विश्लेषण करते हुए कहा है कि—इस प्रकार उस युवती के मन में अपराध भावना घर कर गयी। जब वह चर्च में आती तो वहां के पवित्र वातावरण में यह भावना और उग्र हो उठती थी। परिणाम स्वरूप उसकी रक्त वाहनी की पेशियों से ऐंठन होने लगती और खुजली शुरू हो जाती।
मनःसंस्थान में जमी हुई इस रोग की जड़ों को पहचान कर डा0 पीले ने उक्त युवती को सलाह दी कि वह फर्म के मालिक के सामने सब कुछ स्वीकार कर ले साथ ही चुरायी गयी रकम को अदा करना भी शुरू कर दें। युवती ने नौकरी छूटने का डर बताया तो डा0 पीले ने ढाढ़स बंधाया हो सकता है तुम्हारी फर्म का मालिक तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर तुम्हें नौकरी से न हटाये, पर एक क्षण को यह मान भी लें कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया तो तुम्हें अन्यत्र भी नौकरी मिल सकती है। नौकरी खो देने से उतनी क्षति नहीं होगी जितनी की अपनी आत्मा और आदर्श को खोने से हो रही है।
बात समझ में आ गयी और युवती ने अपने मालिक के पास जाकर सब कुछ कह दिया। वही हुआ जिसकी सुखद सम्भावना डा. पीले ने बतायी थी। अर्थात् मालिक ने उसकी सच्चाई, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के प्रति उदित हुई दृढ़ निष्ठा से प्रभावित होकर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इस क्षमा से युवती का हृदय और पश्चाताप विदग्ध हुआ तथा उसने स्वयं ही वह पद छोड़ दिया। इस पश्चात्ताप और प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप आयी भावनाओं में शुद्धि के कारण युवती को दुबारा फिर कभी खुजली नहीं उठी। इसका कारण यह था, कि उसका भावना-जन्य क्षोभ समाप्त हो चुका था। शरीर की तमाम पेशियां स्नायु मण्डल द्वारा संचलित होती हैं। छोटी मोटी स्नायुओं का एक पूरा जाल मनुष्य शरीर में फैल हुआ है जिसका नियन्त्रण मस्तिष्क से होता है। कुछ स्नायु ऐच्छिक होते हैं, जिनका इच्छानुसार उपयोग होता है जैसे चलना-फिरना या कोई वस्तु पकड़ना छोड़ना। यह कार्य यद्यपि पेशियों द्वारा ही होते हैं, परन्तु पेशियां स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क से ही निर्देश प्राप्त करती हैं। इन ऐच्छिक स्नायुओं के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के स्नायु भी होते हैं जिन्हें अनैच्छिक कहा जाता है। इन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता और ये हृदय के धड़कने, नाड़ियों के फड़कने तथा आंतों के कांपने जैसा कार्य सम्पन्न करते हैं।
इन अनैच्छिक स्नायुओं का नियन्त्रण मस्तिष्क के उस केन्द्र से होता है जिसे ‘हायपोथैल्मस’ कहते हैं। इसी केन्द्र से एक नलिका विहीन ग्रन्थि भी सम्बन्धित रहती है जिसे पिट्यूटरी ग्रन्थि शरीर रक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसिक सन्तुलन को बनाये रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित करती है। पिट्यूटरी ग्रन्थि का आकार यद्यपि एक चने के दाने के बराबर होता है परन्तु यह अन्य नलिका विहीन ग्रन्थियों का भी नियन्त्रण करती है। डा0 पीले ने जिसे युवती का मानसोपचार कर ‘इन्टरनल एक्जिमा’ ठीक किया था वह स्नायुजन्य विकास के कारण ही उत्पन्न हुआ था और भावना-क्षोभ समाप्त होते ही स्वतः ही ठीक भी हो गया।
शरीर के स्वास्थ्य संरक्षण का दायित्व पिट्यूटरी ग्रन्थि ही मुख्य रूप से सम्हालती है डा. एच. सैले ने अपनी शोधों द्वारा यह पता लगाया। यह ग्रन्थि खास तौर से उस समय ज्यादा कमजोर हो जाती है जब व्यक्ति के भीतर भावनात्मक द्वन्द्व, मानसिक उथल पुथल मची हुई हो और ऐसी स्थिति में पेशियों की ऐंठन से लेकर त्वचा विकार, हृदय रोग, पाचन विकार, रक्तचाप से लेकर हमेशा बना रहने वाला सिर दर्द तक पैदा हो सकता है। यह तो सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों का संचालन मस्तिष्क द्वारा भेजे गये निर्देशों से ही होता है। भावनाओं के कारण मस्तिष्क पर अवांछनीय दबाव बना रहेगा तो यह निश्चित ही है कि उसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी हो। अधिकांश रोगों के मूल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भावना क्षोभ ही पाया गया है, भले वह कोई दुराव छिपाव का भाव हो अथवा आक्रोश क्रोध का भाव।