अन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान -1 
निर्मल मन को प्राप्त होती है, ऋतम्भरा प्रज्ञा
Read Scan Version
अन्तःस्थल को निर्मल कर देने वाले अन्तर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त पर अपना प्रभाव डालते हैं। इन प्रयोगों से चित्त की अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं- एक रूपान्तरण की प्रक्रिया घटित होती है। इस प्रक्रिया की तीव्रता के अनुरूप ही परिवर्तित होता है जीवन। चित्त में संस्कार एवं कर्मबीजों की परतों के अनुसार ही जीवन का स्वरूप विकसित होता है। ये विविध संस्कार एवं कर्मबीज काल क्रम में अपनी परिपक्वता के अनुसार ही प्रकट होते हैं। इनके प्रकट होने की अवस्था के अनुरूप ही जीवन की दशा व दिशा बदल जाती है। शुभ संस्कार एवं पुण्य कर्म के प्रकट होने से जहाँ जीवन शुभ व प्रकाश से पूरित होता है, वहीं अशुभ संस्कार एवं पाप कर्म के प्रकट होने से जीवन अशुभ एवं अँधेरे से भर जाता है। योग की वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ- ध्यान के प्रयोग चित्त को उत्तरोत्तर निर्मल बनाते हैं। इससे संस्कारों एवं कर्म बीजों का नाश होने से चित्त आध्यात्मिक ज्योति से ज्योतित होता है व जीवन में आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि होती है।
अन्तस् में आया बदलाव जीवन के समूचे कलेवर एवं परिवेश को बदल देता है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि-
जाको विधि दारुन दुःख देही, ताकी मति पहिले हर लेहीं।
अर्थात् जिसको विधाता दारुण दुःख देना चाहते हैं, उसकी मति का हरण पहले ही कर लेते हैं। स्थिति उलटी भी है-
जाको विधि पूरन सुख देहीं, ताकी मति निर्मल कर देहीं
अर्थात् जिसको विधाता पूर्ण सुख देना चाहते हैं, उसकी मति को निर्मल बना देते हैं।
इस निर्मलता के यौगिक महत्त्व को अगले सूत्र में बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं-
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा॥ १/४८॥
महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में योग साधना की जिन उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, उनमें यह उपलब्धि विशेष है। प्रज्ञा या बौद्धिक चेतना हमारे जीवन रथ की संचालक है। इसकी अवस्था ही जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। सामान्य क्रम में बुद्धि सन्देह, भ्रम की वजह से चंचल रहती है। इस चंचलता की वजह से ही इसकी निर्णय क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता पर असर पड़ता है। बौद्धिक दिशाभ्रम के कारणों में पूर्वाग्रहों, स्वार्थपरता एवं हठधर्मिता का भारी हाथ रहता है। इनके कारण बुद्धि में वह समझदारी नहीं पनप पाती, जिसकी आवश्यकता है।
अन्तर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग- विशेष तौर पर ध्यान की प्रणालियाँ, बुद्धि के इस कल्मष को दूर करती है। इस कल्मष के दूर होने से इसमें सहज निर्मलता आती है। इसके विकार दूर होने से इसमें न केवल सत्य का आकलन करने की योग्यता विकसित होती है, बल्कि इसमें ऋत् दर्शन की दृष्टि भी पनपती है। युगऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं में सत्य के दो रूपों की चर्चा किया करते थे। एक वह जो सामान्य इन्द्रियों एवं साधारण बौद्धिक समझ से देखा व जाना जाता है। जिसके रूप काल एवं परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए टेबल में पुस्तक रखी है। यह सत्य है, किन्तु यह सत्य एक सीमित स्थान एवं सीमित समय के लिए है। समय एवं स्थान के परिवर्तन के साथ ही यह सत्य- सत्य नहीं रह जाएगा।
सत्य के इस सामान्य रूप के अलावा एक अन्य रूप है, जो सर्वकालिकम एवं सार्वभौमिक है। यह अपरिवर्तनीय है। क्योंकि यह किसी एक स्थान से नहीं, बल्कि सम्पूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है। यह सत्य अस्तित्व के नियमों का है। भौतिक ही नहीं, अभौतिक या पराभौतिक प्रकृति इस दायरे में आते हैं। यह न बदलता है और न मिटता है। इसे जानने वाला सृष्टि एवं स्रष्टा के नियमों से परिचित हो जाता है। इसकी प्राप्ति किसी तार्किक अवधारणा या फिर किसी विवेचन, विश्लेषण से नहीं होती। बल्कि इसके लिए सम्पूर्ण अस्तित्व से एक रस होना पड़ता है। और ऐसा तभी होता है, जब योग साधक के चित्त को निर्विकार की भावदशा प्राप्त हो।
ऋतम्भरा में सत्य की शाश्वतता के साथ परमात्मा की सरसता है। रसौ वैः सः की दिव्य अनुभूति इसमें जुड़ी है। यथार्थ में ऋत् है अन्तरतम अस्तित्व, जो हमारा अन्तरतम होने के साथ सभी का अन्तरतम है। जब योगी को निर्विचार समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, तो उसकी प्रज्ञा ऋतम्भरा से आलोकित- आपूरित हो जाती है। उसमें ब्रह्माण्ड की समस्वरता स्पन्दित होने लगती है। यहाँ न कोई द्वन्द्व है और न किसी अव्यवस्था की उलझन। जहाँ कहीं जो भी नकारात्मक है, जो भी विषैला है, वह सबका सब विलीन, विसर्जित हो जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ किसी को निकाल फेंकने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सम्पूर्णता में सबको जीवन के सभी तत्त्वों को उनका अपना स्थान मिल जाता है।
यहाँ पहुँचते ही जीवन चेतना शिकायतों- सन्देहों, उलझनों, भ्रमों से मुक्त हो जाती है। सब कुछ समझ में आने लगता है, एकदम साफ- साफ और सुस्पष्ट। प्रत्येक तत्त्व की स्थिति ही नहीं, उसका औचित्य भी स्पष्ट हो जाता है। और तब पता चलता है कि यथार्थ में परेशान होने का कोई कारण ही नहीं है। यही विशेषता है-इस भावदशा का।
ऋतम्भरा में सर्वत्र सम्पूर्णता ही है। और इस सम्पूर्ण में सभी कुछ इतनी समस्वरता एवं संगीत लिए है कि बस माधुर्य के अलावा कुछ बचता ही नहीं। यहाँ केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु का भी अपूर्व सौन्दर्य है। हर वस्तु नए प्रकाश में आलोकित होता है। पीड़ा भी, दुःख भी एक नए गुणवत्ता के साथ स्वयं को प्रकट करते हैं। यहाँ असुन्दर भी सुन्दर हो जाता है, क्योंकि तब पहली बार समझ में आता है कि विपरीतता, विषमता क्यों आवश्यक है। और तब ये सब और इनमें से कुछ भी असुविधाजनक नहीं रहता। सब का सब एक दूसरे के संपूरक हो जाता है। यह बड़ा ही स्पष्ट अनुभव होता है- ये सभी तत्त्व एक दूसरे की मदद के लिए हैं।
सामान्य बोलचाल में- जिसे हम सब कहते- सुनते हैं, भगवान् का प्रत्येक विधान मंगलमय है। उसकी सही समझ चेतना की इसी अवस्था में समझ आती है। प्रज्ञा के ऋतम्भरा होने पर ही भगवान् के मंगलमय विधान का बोध होता है। अभी वर्तमान में एक कोरा कथन है- जिसमें शब्द तो बोले जाते हैं, परन्तु उनमें कोई अर्थ नहीं होता। बस एक ध्वनि बनकर कानों में गूँज जाती है। इसमें अस्तित्व के प्राण नहीं बसते। परन्तु प्रज्ञा के ऋतम्भरा होने पर इस मंगलमयता की प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभूति होती रहती है। और योगी बन जाता है—मीरा की तरह, सुकरात की भाँति। उसे प्राप्त होती है महात्मा ईसा की अवस्था, जिसमें विष का प्याला, सूली की चुभन भी मंगलमय नजर आती है; क्योंकि तब इसकी बहुमूल्यता अनुभूत होने लगती है।
अन्तस् में आया बदलाव जीवन के समूचे कलेवर एवं परिवेश को बदल देता है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि-
जाको विधि दारुन दुःख देही, ताकी मति पहिले हर लेहीं।
अर्थात् जिसको विधाता दारुण दुःख देना चाहते हैं, उसकी मति का हरण पहले ही कर लेते हैं। स्थिति उलटी भी है-
जाको विधि पूरन सुख देहीं, ताकी मति निर्मल कर देहीं
अर्थात् जिसको विधाता पूर्ण सुख देना चाहते हैं, उसकी मति को निर्मल बना देते हैं।
इस निर्मलता के यौगिक महत्त्व को अगले सूत्र में बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं-
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा॥ १/४८॥
शब्दार्थ-
तत्र= उस समय (योगी की); प्रज्ञा= बुद्धि; ऋतम्भरा= ऋतम्भरा होती है।भावार्थ-
निर्विचार समाधि में प्रज्ञा ऋतम्भरा से सम्पूरित होती है।महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में योग साधना की जिन उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, उनमें यह उपलब्धि विशेष है। प्रज्ञा या बौद्धिक चेतना हमारे जीवन रथ की संचालक है। इसकी अवस्था ही जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। सामान्य क्रम में बुद्धि सन्देह, भ्रम की वजह से चंचल रहती है। इस चंचलता की वजह से ही इसकी निर्णय क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता पर असर पड़ता है। बौद्धिक दिशाभ्रम के कारणों में पूर्वाग्रहों, स्वार्थपरता एवं हठधर्मिता का भारी हाथ रहता है। इनके कारण बुद्धि में वह समझदारी नहीं पनप पाती, जिसकी आवश्यकता है।
अन्तर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग- विशेष तौर पर ध्यान की प्रणालियाँ, बुद्धि के इस कल्मष को दूर करती है। इस कल्मष के दूर होने से इसमें सहज निर्मलता आती है। इसके विकार दूर होने से इसमें न केवल सत्य का आकलन करने की योग्यता विकसित होती है, बल्कि इसमें ऋत् दर्शन की दृष्टि भी पनपती है। युगऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं में सत्य के दो रूपों की चर्चा किया करते थे। एक वह जो सामान्य इन्द्रियों एवं साधारण बौद्धिक समझ से देखा व जाना जाता है। जिसके रूप काल एवं परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए टेबल में पुस्तक रखी है। यह सत्य है, किन्तु यह सत्य एक सीमित स्थान एवं सीमित समय के लिए है। समय एवं स्थान के परिवर्तन के साथ ही यह सत्य- सत्य नहीं रह जाएगा।
सत्य के इस सामान्य रूप के अलावा एक अन्य रूप है, जो सर्वकालिकम एवं सार्वभौमिक है। यह अपरिवर्तनीय है। क्योंकि यह किसी एक स्थान से नहीं, बल्कि सम्पूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है। यह सत्य अस्तित्व के नियमों का है। भौतिक ही नहीं, अभौतिक या पराभौतिक प्रकृति इस दायरे में आते हैं। यह न बदलता है और न मिटता है। इसे जानने वाला सृष्टि एवं स्रष्टा के नियमों से परिचित हो जाता है। इसकी प्राप्ति किसी तार्किक अवधारणा या फिर किसी विवेचन, विश्लेषण से नहीं होती। बल्कि इसके लिए सम्पूर्ण अस्तित्व से एक रस होना पड़ता है। और ऐसा तभी होता है, जब योग साधक के चित्त को निर्विकार की भावदशा प्राप्त हो।
ऋतम्भरा में सत्य की शाश्वतता के साथ परमात्मा की सरसता है। रसौ वैः सः की दिव्य अनुभूति इसमें जुड़ी है। यथार्थ में ऋत् है अन्तरतम अस्तित्व, जो हमारा अन्तरतम होने के साथ सभी का अन्तरतम है। जब योगी को निर्विचार समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, तो उसकी प्रज्ञा ऋतम्भरा से आलोकित- आपूरित हो जाती है। उसमें ब्रह्माण्ड की समस्वरता स्पन्दित होने लगती है। यहाँ न कोई द्वन्द्व है और न किसी अव्यवस्था की उलझन। जहाँ कहीं जो भी नकारात्मक है, जो भी विषैला है, वह सबका सब विलीन, विसर्जित हो जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ किसी को निकाल फेंकने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सम्पूर्णता में सबको जीवन के सभी तत्त्वों को उनका अपना स्थान मिल जाता है।
यहाँ पहुँचते ही जीवन चेतना शिकायतों- सन्देहों, उलझनों, भ्रमों से मुक्त हो जाती है। सब कुछ समझ में आने लगता है, एकदम साफ- साफ और सुस्पष्ट। प्रत्येक तत्त्व की स्थिति ही नहीं, उसका औचित्य भी स्पष्ट हो जाता है। और तब पता चलता है कि यथार्थ में परेशान होने का कोई कारण ही नहीं है। यही विशेषता है-इस भावदशा का।
ऋतम्भरा में सर्वत्र सम्पूर्णता ही है। और इस सम्पूर्ण में सभी कुछ इतनी समस्वरता एवं संगीत लिए है कि बस माधुर्य के अलावा कुछ बचता ही नहीं। यहाँ केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु का भी अपूर्व सौन्दर्य है। हर वस्तु नए प्रकाश में आलोकित होता है। पीड़ा भी, दुःख भी एक नए गुणवत्ता के साथ स्वयं को प्रकट करते हैं। यहाँ असुन्दर भी सुन्दर हो जाता है, क्योंकि तब पहली बार समझ में आता है कि विपरीतता, विषमता क्यों आवश्यक है। और तब ये सब और इनमें से कुछ भी असुविधाजनक नहीं रहता। सब का सब एक दूसरे के संपूरक हो जाता है। यह बड़ा ही स्पष्ट अनुभव होता है- ये सभी तत्त्व एक दूसरे की मदद के लिए हैं।
सामान्य बोलचाल में- जिसे हम सब कहते- सुनते हैं, भगवान् का प्रत्येक विधान मंगलमय है। उसकी सही समझ चेतना की इसी अवस्था में समझ आती है। प्रज्ञा के ऋतम्भरा होने पर ही भगवान् के मंगलमय विधान का बोध होता है। अभी वर्तमान में एक कोरा कथन है- जिसमें शब्द तो बोले जाते हैं, परन्तु उनमें कोई अर्थ नहीं होता। बस एक ध्वनि बनकर कानों में गूँज जाती है। इसमें अस्तित्व के प्राण नहीं बसते। परन्तु प्रज्ञा के ऋतम्भरा होने पर इस मंगलमयता की प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभूति होती रहती है। और योगी बन जाता है—मीरा की तरह, सुकरात की भाँति। उसे प्राप्त होती है महात्मा ईसा की अवस्था, जिसमें विष का प्याला, सूली की चुभन भी मंगलमय नजर आती है; क्योंकि तब इसकी बहुमूल्यता अनुभूत होने लगती है।
Versions
-
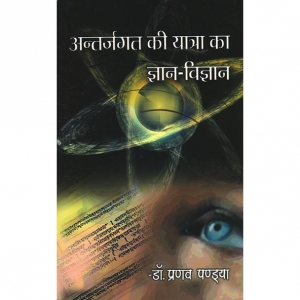
HINDIअन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान-1Text Book Version
-
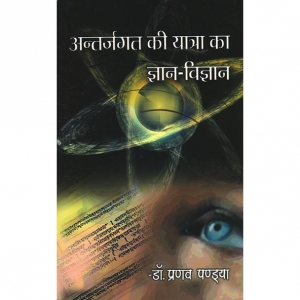
HINDIअन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान -1Text Book Version
-
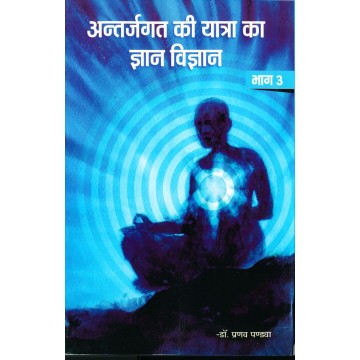
HINDIअन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान -3Scan Book Version
-
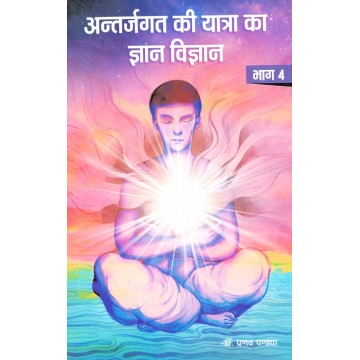
HINDIअन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान -4Scan Book Version
-
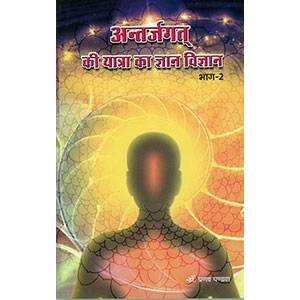
HINDIअन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान -2Scan Book Version
-
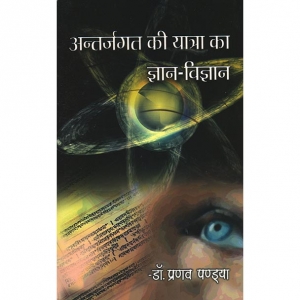
HINDIअन्तर्जगत् की यात्रा का ज्ञान-विज्ञान - 1Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- एक से ही हों एकाकार
- करुणा कर सकती है—चंचल मन पर काबू
- बड़ा गहरा है प्राण व मन का नाता
- ध्यान से उपजती है—अतीन्द्रिय संवेदना
- ध्यान की गहराई में छिपा है—परम सत्य
- राग शमन करता है—वीतराग का ध्यान
- अन्तर्चक्षु खोल देगा निद्रा का मर्म
- अभिरुचि के ही अनुरूप हो ध्यान
- अतिचेतन तक को वश में कर लेता है ध्यान
- स्फटिक मणि सा बनाइये मन
- मंजिल नहीं, पड़ाव है—सवितर्क समाधि
- सत्य का साक्षात्कार है निर्वितर्क समाधि
- ध्यान की अनुभूतियों द्वारा ऊर्जा स्नान
- ध्यान का अगला चरण है—समर्पण
- परम शुद्घ को मिलता है, अध्यात्म का प्रसाद
- निर्मल मन को प्राप्त होती है, ऋतम्भरा प्रज्ञा
- बिन इन्द्रिय जब अनुभूत होता है सत्य
- जब मिलते हैं व्यक्ति और विराट्
- सारे नियंत्रणों पर नियंत्रण है—निर्बीज समाधि

