युगगीता (भाग-४) 
कैसा होना चाहिए योगी का संयत चित्त
Read Scan Version
विनियतं चित्तम्
अठारहवाँ श्लोक कहता है-
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।।
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ ६/१८
अर्थात्- जब (यदा), विशेष रूप से संयत किया हुआ (विनियतं), चित्त (चित्तम्), आत्मा में ही (आत्मनि एव), स्थित रहता है (अवतिष्ठते), तब (तदा), सब प्रकार के काम्य विषयों- आकांक्षाओं से (सर्वकामेभ्यः), कामनारहित (निःस्पृहः), व्यक्ति योग में स्थित है (युक्तः), ऐसा कहा जाता है (इति उच्यते)॥
यह शब्दार्थ हुआ, अब भावार्थ देखते हैं-
अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भाँति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों- कामनाओं से स्पृहारहित (पूर्णतः निस्पृह) पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है ।
भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य कब योग में स्थित है, यह जानना हो तो यह देखना होगा कि वशीभूत चित्त परमात्मा में लगा हुआ है या नहीं एवं उसके मन में भोगों के प्रति निर्लिप्तता का भाव पैदा हुआ या नहीं ।। जब- जब, जिन- जिन क्षणों में, जिस- जिस अवधि में मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है, वह युक्तः- सही अर्थों में एक योगी- एक दिव्यकर्मी कहा जाता है ।। आहार- विहार की अति से बचने की बात कहने के तुरंत बाद वे ध्यानयोग की अति महत्वपूर्ण शर्तें बताते हैं- विनियतं चित्तं- विशेष रूप से संयत किया हुआ चित्त- सारी वृत्तियों को सिकोड़कर एकाग्र किया गया मन तथा फिर कहते हैं- च्च्आत्मनि अवतिष्ठतेज्ज् अर्थात् ऐसा चित्त फिर परमात्मा में ही स्थित हो, इधर- उधर नहीं तथा इसके बाद कहते हैं- निस्पृहः सर्वकामेभ्यः- समस्त कामनाओं की, भोग की कल्पना या इच्छा- आकांक्षा से मुक्त एवं पूर्णतः निस्पृह (कोई भी लगाव न रखने वाला, किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाला) व्यक्ति ही सही मायने में योगी कहलाता है ।।
युक्तः - योगी कौन?
यह वस्तुतः एक प्रकार से व्यावहारिक निर्देश है, जो किसी भी साधक- ध्यानयोगी के लिए जानना जरूरी है ।। एक सच्चा ध्यान करने वाला तभी ध्यान में स्थित कहा जा सकता है, जब उसका मन कामनाओं के द्वारा विक्षुब्ध हो, इधर- उधर न भटक रहा हो ।। जब तक कामनाएँ हैं, विषयभोग की इच्छाएँ हैं, तब तक चित्त लगने वाला है नहीं ।। जैसे ही चित्त संयत हुआ, व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, उसे स्पृहा नहीं परेशान करती, वह अंदर के शुद्ध चैतन्य आत्मतत्त्व में पूर्णतः लीन हो जाता है ।। वहीं तो चिरंतन शांति का निवास है ।। ऐसा व्यक्ति ही भगवान् के अनुसार भली भाँति ध्यान में युक्त माना जा सकता है।
भगवान् यह भी कह रहे हैं कि ध्यान यदि नियमित किया जाए तो चित्त संस्कारशून्य होने लगेगा ।। उच्चस्तरीय चेतना प्रतिबिंबित होने लगेगी ।। बाह्य जगत् में सभी कामनाओं- तामसिकताओं के प्रति अरुचि पैदा होगी व चित्त निर्मल बनेगा ।। ज्यों- ज्यों ध्यान गहरा होता जाता है, चित्त निर्मल होता जाता है ।। इसीलिए नित्य- नियमित ध्यान करते रहना चाहिए ।। जहाँ ध्यान चित्त संयत करने के लिए एक उपचार है, वहाँ ध्यान लगाने की एक आवश्यकता संयत चित्त है, यह तथ्य वे बार- बार समझा रहे हैं ।। प्राणों का रूपांतरण हो तो हमारी वासना व कामना सभी समाप्त हो जाएँ ।। हम प्रयास करें कि हमारी वासना प्रार्थना में बदल जाए।
परमात्मा में स्थित हो करें ध्यान
प्रार्थना भगवान् को देने की प्रक्रिया है ।। प्रार्थना हृदय की गुहा में बैठकर होती है ।। हम हमारा सर्वस्व उसमें उड़ेल देते हैं ।। हमारी संपूर्ण क्रियाशीलता भगवतसत्ता के चरणों में अर्पित हो जाती है; जबकि वासना की पूर्ति बिना दूसरे व्यक्ति के नहीं हो सकती है ।। इसलिए यदि हम परमात्मा में स्थित होकर ध्यान करते हैं तो स्वतः हमारा चित्त संयत हो जाता है- वासनाएँ रूपांतरित हो जाती हैं- हमारे मुख से फिर प्रार्थना ही निकलती है- मन भगवान् को ही अर्पित हो जाते हैं- चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है; क्योंकि गिराने वाले तत्त्व अब रूपांतरित हो गए हैं ।। इसके लिए निस्पृहता का गुण होना साधक के लिए अनिवार्य है ।। यदि वह हर कार्यों में अपनी हर चेष्टा में निस्पृह है, तो फिर आसक्ति उससे दूर रहेगी, वह निर्लिप्त भाव से यज्ञीय जीवन जिएगा एवं जैसा कि श्रीकृष्ण ने कहा है कि फिर वह परमात्मा में ही स्थित बना रह सही अर्थों में योगी कहलाएगा ।। श्रीकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि जिस भाग्यवान पुरुष से यह आत्मसंयम वाला कर्मयोग सध जाए, वह मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित हो जाता है ।।
परमपूज्य गुरुदेव इसी प्रसंग पर लिखते हैं- जिस युग में, जिस समाज के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसमें अवांछनीय प्रचलनों की कमी नहीं ।। उनका आकर्षण मन को अपनी ओर खींचता- लुभाता है ।। पानी स्वभावतः नीचे गिरता है ।। तत्काल लाभ की बात सहज ही मन को आकर्षित करती है और दबी हुई दुष्प्रवृत्तियाँ उभरकर उस मार्ग पर घसीट ले जाती हैं, जो मनुष्य जैसे विवेकी प्राणी के लिए अशोभनीय है ।। योग- साधना मूलतः इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रचंड संघर्ष खड़ा कर देती है ।। जिस महाभारत में श्रीकृष्ण और अर्जुन ने सम्मिलित भूमिका निभाई थी, वह आत्मपरिष्कार में योग- साधना के साथ पूरी तरह से संबंधित है ।। कुसंस्कार कौरव दल से कम नहीं ।। वे निकृष्ट योनियों के साथ चले आ रहे हैं और वातावरण में घुसी अवांछनीयताओं से उद्दीप्त हो भड़कते रहते हैं ।। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों की सारी संपदा हथिया ली थी एवं वापस लेने के लिए पांडवों को युद्ध करना पड़ा, ठीक इसी तरह से आत्मिक गरिमा पर असुरता आच्छादित हो रही है ।। उसको इस चंगुल से छुड़ाने के लिए विरोध- प्रतिरोध का महाभारत खड़ा करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया है ।। योगाभ्यास में इसी विरोध्- संघर्ष का उल्लेख है ।। इसमें आत्मा- परमात्मा, सत्कर्म व सद्ज्ञान का समन्वय करने पर विजय सर्वथा निश्चित हो जाती है । (साधना पद्धतियों का ज्ञान- विज्ञानज् वाङ्मय खंड ४, पृष्ठ १.१२३)
एक अति सुंदर उपमा
इस प्रकार जब भली भाँति संयत चित्त हो सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही विश्राम पाता है, तब ऐसा माना जा सकता है कि योगी ने ध्यान में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली है ।। यह एक प्रकार से ध्यानयोग में प्रगति की समीक्षा है, जो श्रीकृष्ण ने अठारहवें श्लोक में की है; किंतु यह स्पष्ट होना जरूरी है कि मन व चित्त को संयत कर ध्यान को आत्मसत्ता के साथ कैसे पूर्णतः लीन करना है ।। इसके लिए भगवान् एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर अगले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं-
यथा दीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यतचित्तस्य युज्जतो योगमात्मनः ॥ -६/१९
शब्दार्थ -- जिस प्रकार (यथा), दीपक (दीपः), वायुरहित स्थान में (निवातस्थः), जरा भी कंपित नहीं होता (न इंगते), आत्मा का (आत्मनः), निरोध- योग (योगम्), युक्त होने वाले (युज्जतः), संयतचित्त योगी की (यतचित्तस्य योगिनः), वही (सा), उपमा (तुलना) उसी रूप में जानना (स्मृता) ।।
भावार्थ हुआ- जैसे सुरक्षित वायुरहित स्थान में रखे दीपक की लौ नहीं डोलती- यही उपमा योग के अभ्यास में लगे योगी के संयत चित्त की अवस्था की ओर संकेत करने के लिए दी गई है ।। (परमात्मा के ध्यान में लगे योगी का जीता हुआ चित्त ऐसा ही होता है।)
कितनी सुंदर उपमा है- एक साधारण- सा व्यक्ति भी समझ सके, वह उदाहरण श्रीकृष्ण ने यहाँ दिया है ।। मन ऐसा हो कि जरा भी डगमगाने न पाए, जरा भी चित्तरूपी लौ प्रकंपित न हो ।। हमारे ऋषिगण योगी के संयत चित्त की अवस्था की ओर संकेत करने के लिए इसी तरह का उदाहरण देते रहे हैं ।। संयत चित्तज् (विनियतं चित्तं) जिसकी बात १८वें श्लोक में कही, अब भगवान् उदाहरण सहित उसे समझा रहे हैं ।। सामान्यतः दीपक जब वायुरहित स्थान पर रखा जाता है एवं इसकी लौ पर त्राटक किया जाता है तो इसके न हिलने के कारण मन क्रमशः बहिर्त्राटक- अंतःत्राटक प्रक्रिया द्वारा स्थिर हो जाता है। परमपूज्य गुरुदेव ने इसे ज्योति- अवतरण की साधना नाम दिया है ।। दीपक का यह ध्यान बड़ा ही पवित्र- आज्ञाचक्र का जागरण करने वाला तथा चित्त को जीत लेने वाला, काम- वासनाओं का हरण करने वाला बताया जाता है ।। संभवतः श्रीकृष्ण को इससे सुंदर कोई उदाहरण नहीं मिला ।। चित्त को संयत करने के लिए वे कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, जैसी कि उस दीपक की लौ की होती है, जो जरा भी डगमगाए नहीं, सीधी- स्थिर हो प्रखर बनी रहे। चित्त भी इसी तरह डोले नहीं, इधर- उधर न भागे ।।
निष्कंप लौ की तरह हो चित्त
वैसे दीपक की लौ को यदि हम सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखें तो पाएँगे कि उसका यह नृत्य इतना तेज गति से होता है कि वह देखने में स्थिर ही दिखाई देता है ।। आधुनिक भौतिकीवादि इस तथ्य को स्थापित कर चुके हैं ।। लेकिन हमारे ऋषिगण ध्यान के लिए उसी लौ की बात कहते रहे हैं, जो निष्कंप अवस्था में वायुरहित स्थान पर दीपक की बाती से निकलती हमें दिखाई देती है ।। सांसारिक कामोद्वेग- आकांक्षाओं और अहंता की आँधियाँ हमारे अंतःकरण चतुष्टय को निरंतर प्रभावित करती हैं ।। हमारा मन व बुद्धि उसके प्रभावों से बच नहीं पाते ।। जब हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा मन व चित्त स्थिर है, इन झोकों में हट नहीं रहा ।। यदि वास्तव में ऐसा होता है, तब हम अपने आप को ध्यान में स्थित मान सकते हैं ।।
कब होता है चित्त असंयत
मन हमारा तीन ही प्रकार की स्थितियों में उद्विग्न व विक्षुब्ध होता है- काम, लोभ एवं अहं ।। इन्हीं को वासना, तृष्णा एवं अहंता कहा गया है ।। काम की पूर्णता में- कामुकता की पूर्ति में व्यवधान आता है, तो वही क्रोध बन जाता है ।। तृष्णा- लालच आज बहुत अधिक बढ़ा- चढ़ा है; क्योंकि हम भोगवादी समाज में जी रहे हैं ।। नकल व प्रतिद्वंद्विता भी व्यक्ति से नादानी कराती दीखती है ।। सबसे बड़ी फुफकारने वाली नागिन अहं की है ।। अहंज् की टकराहट ने ही ढेरों द्वंद्वों को एवं अच्छी- खासी प्रतिभाओं को मिट्टी में मिलते देखा है ।। अहं और कुछ नहीं, यह मान्यता है कि सृष्टि का केंद्र मैं हूँ, कोई और नहीं ।। किसी भी दिव्यकर्मी- साधक के मार्ग की बाधाएँ ये तीन ही हैं; क्योंकि इन्हीं के कारण चित्त असंयत होता रहता है एवं मन- बुद्धि अंतस् के दीपक की शिखा- लौ रहती है ।। जब तक ऐसा होगा, मन कैसे लगेगा ?? इसीलिए सभी ऋषिगण, विद्वज्जन एवं श्रीकृष्ण जैसे योग मनीषी बार- बार यही राय देते रहे हैं कि इनसे बचो; क्योंकि ये रजोगुण की वृद्धि कर व्यक्ति को तमोगुणी बनाते हैं ।। समाजसेवा में भी ये ही तीन बाधाएँ हैं, जो किसी के अंदर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करने में एक प्रकार से विघ्र बनती हैं ।। यह बात बार- बार श्रीकृष्ण ने काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवःज् (तीसरे अध्याय का ३७वाँ श्लोक) तथा त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, (सोलहवें अध्याय का २१वाँ श्लोक) के माध्यम से कही है ।। जो व्यक्ति इन तीनों को भी पालेगा तथा योगी भी बनने का प्रयास करेगा, वह एक प्रकार से अधोगति को ही प्राप्त हो रहा होगा; क्योंकि ऊपर का द्वार तो उसके लिए खुलने वाला है नहीं ।।
बाधक आँधियाँ
ध्यान हेतु सबसे बड़ी जरूरत है- संयत चित्तज् एवं वह भी आत्मनि अवतिष्ठतेज् हो- परमात्मा में लगा हुआ हो तथा सभी प्रकार के काम्य विषयों के प्रति वह पूर्णतः वासनारहित, आसक्तिरहित (निस्पृह) हो, निर्लोभ हो, तभी उस व्यक्ति के ध्यानयोग में प्रवृत्त होने की बात कही जा सकती है। निस्पृहता में एवं चित्त की संयतता में बाधक हैं वे आँधियाँ, जिनका जिक्र ऊपर किया गया ।। जो इन तीन खाइयों को पार करके छलाँग लगाकर बाहर आ गया, वह जीवन- समर का पहला सोपान पार कर गया, पर अधिकांश तो इन्हीं तीन में उलझकर सारा जीवन पुत्रैषणा (वासना), वित्तैषणा (तृष्णा) एवं लोकैषणा (अहंता) में- इनकी पूर्ति में ही बिताते देखे जाते हैं ।। ध्यान में मन लगे तो कैसे ??
दुःखनाशक योग ही हो हम सबका लक्ष्य
श्रीकृष्ण चाहते हैं कि ध्यान में अर्जुन जैसा साधक प्रवृत्त हो; क्योंकि योग ही ऐसी प्रक्रिया है, जो दुःखनाशक है (योगो भवति दुःखहा) ।। अर्जुन विषाद योग से पीड़ित है एवं हम सभी ९९.९ प्रतिशत धरती पर रहने वाले लोग भी इस कष्ट से गुजर रहे हैं ।। अंदर के अनुभव- निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मन हमारा छलाँग लगाना चाहता है- दिव्य चैतन्य अवस्था की प्राप्ति उसकी अभिलाषा है ।। वह बार- बार कहता है कि वही सच्चिदानंद मैं हूँ- एकोऽहम् द्विऽतीयोनास्ति- सोऽहम्, किंतु वह यह नहीं जानता कि इस छलाँग के लिए उसका ऊर्ध्वगामी होना, दीपशिखा की तरह निष्कंप होकर किसी भी प्रकार के झंझावातों से सुरक्षित रहना, कितना जरूरी है ।। जैसे- जैसे ध्यान में यह स्थिरता बढ़ती है, वैसे- वैसे निर्लिप्तता- निरासक्ति, निस्पृहता बढ़ती जाती है- अपरिग्रह एवं विनम्रता आती जाती है ।। व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है एवं प्रचंड मनोबल से ओतप्रोत हम हो चुके होते हैं ।। फिर ध्यान तो सफल होगा ही ।। परमपूज्य गुरुदेव लिखते हैं-च्च्वासनाएँ आदमी को नींबू की तरह निचोड़ लेती हैं ।
जीवन में से स्वास्थ्य, संतुलन, आयुष्य जैसा सब कुछ निचोड़कर उसे छिलके जैसा निस्तेज बनाकर रख देती हैं । तृष्णाओं की खाई इतनी गहरी है कि जिसे रावण, हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर जैसे प्रबल पराक्रमी भी समूचा पौरुष दाँव पर लगा देने के बाद भी पाट सकने में तनिक भी समर्थ न हुए । अहंकार प्रदर्शित करने के दर्प में संसार भर को चुनौती देने और ताल ठोकने वाले किसी समय के दुर्दांत में से अब कोई नहीं दीख पड़ता । राजाओं के मणिमुक्तकों से जड़े राजमुकुट और सिंहासन जाने धराशायी होकर कहाँ धूल चाट रहे होंगे ?ज्ज् (च्जीवन देवता की साधना-आराधनाज्-वाङ्मय खण्ड २, पृष्ठ नं ३.४) । बड़ा ही स्पष्ट चिंतन है । हम इन दुष्प्रवृत्तियों से उबरें एवं मानव जीवन की गरिमा समझें । एक श्रेष्ठ कर्मयोगी बनें । ध्यान द्वारा आत्मोत्कर्ष करें, यही श्रीकृष्ण की भी तो इच्छा है ।
कामनाओं से मुक्ति ही सिद्घि का राजमार्ग
सर एडविन अर्नाल्ड ने पुस्तक लिखी है-च्लाइट ऑफ एशियाज् । उसमें वे लिखते हैं कि बुद्ध को सतत देववाणी सुनाई पड़ती थी सोते-जागते । वह यही कहती कि जब तक कामनाओं के संसार से नहीं निकल जाते, तब तक अनुभूति नहीं होगी, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इन्हीं देववाणियों ने उन्हें कामनाओं के जाल से निकाला एवं वे सारी भोग-वासनाओं को लात मारकर गौतम बुद्ध हो गए । हर व्यक्ति के अंदर ये संभावनाएँ छिपी पड़ी हैं । समस्या यही है कि हम अपने आप को ही सुन नहीं पाते । औरों को सुन लेते हैं । सभी कुछ मुग्ध करने वाले दृश्य देख लेते हैं, उनमें आसक्ति भी पैदा कर लेते हैं, पर अपनी आत्मसत्ता से निस्सृत हो रही देववाणी नहीं सुन पाते । शिष्यत्व का एक प्रमुख लक्षण है-इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का त्याग । जिसने अपनी कामनाएँ छोड़ दीं, उसका मन-चित्त संयत हो गया और फिर वह परमात्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गया । गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं-च्च्कहऊँ कवन सिधि लोक रिझाए।ज्ज् तुम खुद सोचो कि लोक को रिझाकर कौन-सी सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी । फिर न जाने क्यों हम बार-बार उसी मार्ग पर चले जाते हैं। ऋषियों के अनुसार यही माया है ।
गीता के छठे अध्याय के इन दोनों श्लोकों-१८वें व १९वें का मर्म यही है कि ध्यान सफल तब ही होगा, जब हम कामनाओं के जाल से निकलेंगे । ध्यान अपने चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया भी है तथा उस ध्यान को कैसे किया जाए, इसके लिए श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे दैनंदिन जीवन का है-हमारी पूजास्थली में वायुरहित स्थान पर रखा एक दीपक, जिसकी ज्योति निरंतर प्रज्वलित है, निष्कंप है एवं हमें, हमारे चित्त को भी इस संसार-सागर में वैसा ही बनाए रखने की प्रेरणा देती है । हम कितने ही बुद्धिवादी हों, शास्त्रज्ञान जानते हों, यह स्पष्ट मान लें कि उससे आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं । बुद्घि के बंधनों-वासना, तृष्णा, अहंताओं से ऊपर जाकर ही हम शुद्ध आनंदमय चैतन्य को पा सकते हैं ।
अठारहवाँ श्लोक कहता है-
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।।
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ ६/१८
अर्थात्- जब (यदा), विशेष रूप से संयत किया हुआ (विनियतं), चित्त (चित्तम्), आत्मा में ही (आत्मनि एव), स्थित रहता है (अवतिष्ठते), तब (तदा), सब प्रकार के काम्य विषयों- आकांक्षाओं से (सर्वकामेभ्यः), कामनारहित (निःस्पृहः), व्यक्ति योग में स्थित है (युक्तः), ऐसा कहा जाता है (इति उच्यते)॥
यह शब्दार्थ हुआ, अब भावार्थ देखते हैं-
अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भाँति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों- कामनाओं से स्पृहारहित (पूर्णतः निस्पृह) पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है ।
भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य कब योग में स्थित है, यह जानना हो तो यह देखना होगा कि वशीभूत चित्त परमात्मा में लगा हुआ है या नहीं एवं उसके मन में भोगों के प्रति निर्लिप्तता का भाव पैदा हुआ या नहीं ।। जब- जब, जिन- जिन क्षणों में, जिस- जिस अवधि में मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है, वह युक्तः- सही अर्थों में एक योगी- एक दिव्यकर्मी कहा जाता है ।। आहार- विहार की अति से बचने की बात कहने के तुरंत बाद वे ध्यानयोग की अति महत्वपूर्ण शर्तें बताते हैं- विनियतं चित्तं- विशेष रूप से संयत किया हुआ चित्त- सारी वृत्तियों को सिकोड़कर एकाग्र किया गया मन तथा फिर कहते हैं- च्च्आत्मनि अवतिष्ठतेज्ज् अर्थात् ऐसा चित्त फिर परमात्मा में ही स्थित हो, इधर- उधर नहीं तथा इसके बाद कहते हैं- निस्पृहः सर्वकामेभ्यः- समस्त कामनाओं की, भोग की कल्पना या इच्छा- आकांक्षा से मुक्त एवं पूर्णतः निस्पृह (कोई भी लगाव न रखने वाला, किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाला) व्यक्ति ही सही मायने में योगी कहलाता है ।।
युक्तः - योगी कौन?
यह वस्तुतः एक प्रकार से व्यावहारिक निर्देश है, जो किसी भी साधक- ध्यानयोगी के लिए जानना जरूरी है ।। एक सच्चा ध्यान करने वाला तभी ध्यान में स्थित कहा जा सकता है, जब उसका मन कामनाओं के द्वारा विक्षुब्ध हो, इधर- उधर न भटक रहा हो ।। जब तक कामनाएँ हैं, विषयभोग की इच्छाएँ हैं, तब तक चित्त लगने वाला है नहीं ।। जैसे ही चित्त संयत हुआ, व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, उसे स्पृहा नहीं परेशान करती, वह अंदर के शुद्ध चैतन्य आत्मतत्त्व में पूर्णतः लीन हो जाता है ।। वहीं तो चिरंतन शांति का निवास है ।। ऐसा व्यक्ति ही भगवान् के अनुसार भली भाँति ध्यान में युक्त माना जा सकता है।
भगवान् यह भी कह रहे हैं कि ध्यान यदि नियमित किया जाए तो चित्त संस्कारशून्य होने लगेगा ।। उच्चस्तरीय चेतना प्रतिबिंबित होने लगेगी ।। बाह्य जगत् में सभी कामनाओं- तामसिकताओं के प्रति अरुचि पैदा होगी व चित्त निर्मल बनेगा ।। ज्यों- ज्यों ध्यान गहरा होता जाता है, चित्त निर्मल होता जाता है ।। इसीलिए नित्य- नियमित ध्यान करते रहना चाहिए ।। जहाँ ध्यान चित्त संयत करने के लिए एक उपचार है, वहाँ ध्यान लगाने की एक आवश्यकता संयत चित्त है, यह तथ्य वे बार- बार समझा रहे हैं ।। प्राणों का रूपांतरण हो तो हमारी वासना व कामना सभी समाप्त हो जाएँ ।। हम प्रयास करें कि हमारी वासना प्रार्थना में बदल जाए।
परमात्मा में स्थित हो करें ध्यान
प्रार्थना भगवान् को देने की प्रक्रिया है ।। प्रार्थना हृदय की गुहा में बैठकर होती है ।। हम हमारा सर्वस्व उसमें उड़ेल देते हैं ।। हमारी संपूर्ण क्रियाशीलता भगवतसत्ता के चरणों में अर्पित हो जाती है; जबकि वासना की पूर्ति बिना दूसरे व्यक्ति के नहीं हो सकती है ।। इसलिए यदि हम परमात्मा में स्थित होकर ध्यान करते हैं तो स्वतः हमारा चित्त संयत हो जाता है- वासनाएँ रूपांतरित हो जाती हैं- हमारे मुख से फिर प्रार्थना ही निकलती है- मन भगवान् को ही अर्पित हो जाते हैं- चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है; क्योंकि गिराने वाले तत्त्व अब रूपांतरित हो गए हैं ।। इसके लिए निस्पृहता का गुण होना साधक के लिए अनिवार्य है ।। यदि वह हर कार्यों में अपनी हर चेष्टा में निस्पृह है, तो फिर आसक्ति उससे दूर रहेगी, वह निर्लिप्त भाव से यज्ञीय जीवन जिएगा एवं जैसा कि श्रीकृष्ण ने कहा है कि फिर वह परमात्मा में ही स्थित बना रह सही अर्थों में योगी कहलाएगा ।। श्रीकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि जिस भाग्यवान पुरुष से यह आत्मसंयम वाला कर्मयोग सध जाए, वह मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित हो जाता है ।।
परमपूज्य गुरुदेव इसी प्रसंग पर लिखते हैं- जिस युग में, जिस समाज के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसमें अवांछनीय प्रचलनों की कमी नहीं ।। उनका आकर्षण मन को अपनी ओर खींचता- लुभाता है ।। पानी स्वभावतः नीचे गिरता है ।। तत्काल लाभ की बात सहज ही मन को आकर्षित करती है और दबी हुई दुष्प्रवृत्तियाँ उभरकर उस मार्ग पर घसीट ले जाती हैं, जो मनुष्य जैसे विवेकी प्राणी के लिए अशोभनीय है ।। योग- साधना मूलतः इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रचंड संघर्ष खड़ा कर देती है ।। जिस महाभारत में श्रीकृष्ण और अर्जुन ने सम्मिलित भूमिका निभाई थी, वह आत्मपरिष्कार में योग- साधना के साथ पूरी तरह से संबंधित है ।। कुसंस्कार कौरव दल से कम नहीं ।। वे निकृष्ट योनियों के साथ चले आ रहे हैं और वातावरण में घुसी अवांछनीयताओं से उद्दीप्त हो भड़कते रहते हैं ।। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों की सारी संपदा हथिया ली थी एवं वापस लेने के लिए पांडवों को युद्ध करना पड़ा, ठीक इसी तरह से आत्मिक गरिमा पर असुरता आच्छादित हो रही है ।। उसको इस चंगुल से छुड़ाने के लिए विरोध- प्रतिरोध का महाभारत खड़ा करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया है ।। योगाभ्यास में इसी विरोध्- संघर्ष का उल्लेख है ।। इसमें आत्मा- परमात्मा, सत्कर्म व सद्ज्ञान का समन्वय करने पर विजय सर्वथा निश्चित हो जाती है । (साधना पद्धतियों का ज्ञान- विज्ञानज् वाङ्मय खंड ४, पृष्ठ १.१२३)
एक अति सुंदर उपमा
इस प्रकार जब भली भाँति संयत चित्त हो सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही विश्राम पाता है, तब ऐसा माना जा सकता है कि योगी ने ध्यान में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली है ।। यह एक प्रकार से ध्यानयोग में प्रगति की समीक्षा है, जो श्रीकृष्ण ने अठारहवें श्लोक में की है; किंतु यह स्पष्ट होना जरूरी है कि मन व चित्त को संयत कर ध्यान को आत्मसत्ता के साथ कैसे पूर्णतः लीन करना है ।। इसके लिए भगवान् एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर अगले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं-
यथा दीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यतचित्तस्य युज्जतो योगमात्मनः ॥ -६/१९
शब्दार्थ -- जिस प्रकार (यथा), दीपक (दीपः), वायुरहित स्थान में (निवातस्थः), जरा भी कंपित नहीं होता (न इंगते), आत्मा का (आत्मनः), निरोध- योग (योगम्), युक्त होने वाले (युज्जतः), संयतचित्त योगी की (यतचित्तस्य योगिनः), वही (सा), उपमा (तुलना) उसी रूप में जानना (स्मृता) ।।
भावार्थ हुआ- जैसे सुरक्षित वायुरहित स्थान में रखे दीपक की लौ नहीं डोलती- यही उपमा योग के अभ्यास में लगे योगी के संयत चित्त की अवस्था की ओर संकेत करने के लिए दी गई है ।। (परमात्मा के ध्यान में लगे योगी का जीता हुआ चित्त ऐसा ही होता है।)
कितनी सुंदर उपमा है- एक साधारण- सा व्यक्ति भी समझ सके, वह उदाहरण श्रीकृष्ण ने यहाँ दिया है ।। मन ऐसा हो कि जरा भी डगमगाने न पाए, जरा भी चित्तरूपी लौ प्रकंपित न हो ।। हमारे ऋषिगण योगी के संयत चित्त की अवस्था की ओर संकेत करने के लिए इसी तरह का उदाहरण देते रहे हैं ।। संयत चित्तज् (विनियतं चित्तं) जिसकी बात १८वें श्लोक में कही, अब भगवान् उदाहरण सहित उसे समझा रहे हैं ।। सामान्यतः दीपक जब वायुरहित स्थान पर रखा जाता है एवं इसकी लौ पर त्राटक किया जाता है तो इसके न हिलने के कारण मन क्रमशः बहिर्त्राटक- अंतःत्राटक प्रक्रिया द्वारा स्थिर हो जाता है। परमपूज्य गुरुदेव ने इसे ज्योति- अवतरण की साधना नाम दिया है ।। दीपक का यह ध्यान बड़ा ही पवित्र- आज्ञाचक्र का जागरण करने वाला तथा चित्त को जीत लेने वाला, काम- वासनाओं का हरण करने वाला बताया जाता है ।। संभवतः श्रीकृष्ण को इससे सुंदर कोई उदाहरण नहीं मिला ।। चित्त को संयत करने के लिए वे कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए, जैसी कि उस दीपक की लौ की होती है, जो जरा भी डगमगाए नहीं, सीधी- स्थिर हो प्रखर बनी रहे। चित्त भी इसी तरह डोले नहीं, इधर- उधर न भागे ।।
निष्कंप लौ की तरह हो चित्त
वैसे दीपक की लौ को यदि हम सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखें तो पाएँगे कि उसका यह नृत्य इतना तेज गति से होता है कि वह देखने में स्थिर ही दिखाई देता है ।। आधुनिक भौतिकीवादि इस तथ्य को स्थापित कर चुके हैं ।। लेकिन हमारे ऋषिगण ध्यान के लिए उसी लौ की बात कहते रहे हैं, जो निष्कंप अवस्था में वायुरहित स्थान पर दीपक की बाती से निकलती हमें दिखाई देती है ।। सांसारिक कामोद्वेग- आकांक्षाओं और अहंता की आँधियाँ हमारे अंतःकरण चतुष्टय को निरंतर प्रभावित करती हैं ।। हमारा मन व बुद्धि उसके प्रभावों से बच नहीं पाते ।। जब हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा मन व चित्त स्थिर है, इन झोकों में हट नहीं रहा ।। यदि वास्तव में ऐसा होता है, तब हम अपने आप को ध्यान में स्थित मान सकते हैं ।।
कब होता है चित्त असंयत
मन हमारा तीन ही प्रकार की स्थितियों में उद्विग्न व विक्षुब्ध होता है- काम, लोभ एवं अहं ।। इन्हीं को वासना, तृष्णा एवं अहंता कहा गया है ।। काम की पूर्णता में- कामुकता की पूर्ति में व्यवधान आता है, तो वही क्रोध बन जाता है ।। तृष्णा- लालच आज बहुत अधिक बढ़ा- चढ़ा है; क्योंकि हम भोगवादी समाज में जी रहे हैं ।। नकल व प्रतिद्वंद्विता भी व्यक्ति से नादानी कराती दीखती है ।। सबसे बड़ी फुफकारने वाली नागिन अहं की है ।। अहंज् की टकराहट ने ही ढेरों द्वंद्वों को एवं अच्छी- खासी प्रतिभाओं को मिट्टी में मिलते देखा है ।। अहं और कुछ नहीं, यह मान्यता है कि सृष्टि का केंद्र मैं हूँ, कोई और नहीं ।। किसी भी दिव्यकर्मी- साधक के मार्ग की बाधाएँ ये तीन ही हैं; क्योंकि इन्हीं के कारण चित्त असंयत होता रहता है एवं मन- बुद्धि अंतस् के दीपक की शिखा- लौ रहती है ।। जब तक ऐसा होगा, मन कैसे लगेगा ?? इसीलिए सभी ऋषिगण, विद्वज्जन एवं श्रीकृष्ण जैसे योग मनीषी बार- बार यही राय देते रहे हैं कि इनसे बचो; क्योंकि ये रजोगुण की वृद्धि कर व्यक्ति को तमोगुणी बनाते हैं ।। समाजसेवा में भी ये ही तीन बाधाएँ हैं, जो किसी के अंदर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करने में एक प्रकार से विघ्र बनती हैं ।। यह बात बार- बार श्रीकृष्ण ने काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवःज् (तीसरे अध्याय का ३७वाँ श्लोक) तथा त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, (सोलहवें अध्याय का २१वाँ श्लोक) के माध्यम से कही है ।। जो व्यक्ति इन तीनों को भी पालेगा तथा योगी भी बनने का प्रयास करेगा, वह एक प्रकार से अधोगति को ही प्राप्त हो रहा होगा; क्योंकि ऊपर का द्वार तो उसके लिए खुलने वाला है नहीं ।।
बाधक आँधियाँ
ध्यान हेतु सबसे बड़ी जरूरत है- संयत चित्तज् एवं वह भी आत्मनि अवतिष्ठतेज् हो- परमात्मा में लगा हुआ हो तथा सभी प्रकार के काम्य विषयों के प्रति वह पूर्णतः वासनारहित, आसक्तिरहित (निस्पृह) हो, निर्लोभ हो, तभी उस व्यक्ति के ध्यानयोग में प्रवृत्त होने की बात कही जा सकती है। निस्पृहता में एवं चित्त की संयतता में बाधक हैं वे आँधियाँ, जिनका जिक्र ऊपर किया गया ।। जो इन तीन खाइयों को पार करके छलाँग लगाकर बाहर आ गया, वह जीवन- समर का पहला सोपान पार कर गया, पर अधिकांश तो इन्हीं तीन में उलझकर सारा जीवन पुत्रैषणा (वासना), वित्तैषणा (तृष्णा) एवं लोकैषणा (अहंता) में- इनकी पूर्ति में ही बिताते देखे जाते हैं ।। ध्यान में मन लगे तो कैसे ??
दुःखनाशक योग ही हो हम सबका लक्ष्य
श्रीकृष्ण चाहते हैं कि ध्यान में अर्जुन जैसा साधक प्रवृत्त हो; क्योंकि योग ही ऐसी प्रक्रिया है, जो दुःखनाशक है (योगो भवति दुःखहा) ।। अर्जुन विषाद योग से पीड़ित है एवं हम सभी ९९.९ प्रतिशत धरती पर रहने वाले लोग भी इस कष्ट से गुजर रहे हैं ।। अंदर के अनुभव- निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मन हमारा छलाँग लगाना चाहता है- दिव्य चैतन्य अवस्था की प्राप्ति उसकी अभिलाषा है ।। वह बार- बार कहता है कि वही सच्चिदानंद मैं हूँ- एकोऽहम् द्विऽतीयोनास्ति- सोऽहम्, किंतु वह यह नहीं जानता कि इस छलाँग के लिए उसका ऊर्ध्वगामी होना, दीपशिखा की तरह निष्कंप होकर किसी भी प्रकार के झंझावातों से सुरक्षित रहना, कितना जरूरी है ।। जैसे- जैसे ध्यान में यह स्थिरता बढ़ती है, वैसे- वैसे निर्लिप्तता- निरासक्ति, निस्पृहता बढ़ती जाती है- अपरिग्रह एवं विनम्रता आती जाती है ।। व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है एवं प्रचंड मनोबल से ओतप्रोत हम हो चुके होते हैं ।। फिर ध्यान तो सफल होगा ही ।। परमपूज्य गुरुदेव लिखते हैं-च्च्वासनाएँ आदमी को नींबू की तरह निचोड़ लेती हैं ।
जीवन में से स्वास्थ्य, संतुलन, आयुष्य जैसा सब कुछ निचोड़कर उसे छिलके जैसा निस्तेज बनाकर रख देती हैं । तृष्णाओं की खाई इतनी गहरी है कि जिसे रावण, हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर जैसे प्रबल पराक्रमी भी समूचा पौरुष दाँव पर लगा देने के बाद भी पाट सकने में तनिक भी समर्थ न हुए । अहंकार प्रदर्शित करने के दर्प में संसार भर को चुनौती देने और ताल ठोकने वाले किसी समय के दुर्दांत में से अब कोई नहीं दीख पड़ता । राजाओं के मणिमुक्तकों से जड़े राजमुकुट और सिंहासन जाने धराशायी होकर कहाँ धूल चाट रहे होंगे ?ज्ज् (च्जीवन देवता की साधना-आराधनाज्-वाङ्मय खण्ड २, पृष्ठ नं ३.४) । बड़ा ही स्पष्ट चिंतन है । हम इन दुष्प्रवृत्तियों से उबरें एवं मानव जीवन की गरिमा समझें । एक श्रेष्ठ कर्मयोगी बनें । ध्यान द्वारा आत्मोत्कर्ष करें, यही श्रीकृष्ण की भी तो इच्छा है ।
कामनाओं से मुक्ति ही सिद्घि का राजमार्ग
सर एडविन अर्नाल्ड ने पुस्तक लिखी है-च्लाइट ऑफ एशियाज् । उसमें वे लिखते हैं कि बुद्ध को सतत देववाणी सुनाई पड़ती थी सोते-जागते । वह यही कहती कि जब तक कामनाओं के संसार से नहीं निकल जाते, तब तक अनुभूति नहीं होगी, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इन्हीं देववाणियों ने उन्हें कामनाओं के जाल से निकाला एवं वे सारी भोग-वासनाओं को लात मारकर गौतम बुद्ध हो गए । हर व्यक्ति के अंदर ये संभावनाएँ छिपी पड़ी हैं । समस्या यही है कि हम अपने आप को ही सुन नहीं पाते । औरों को सुन लेते हैं । सभी कुछ मुग्ध करने वाले दृश्य देख लेते हैं, उनमें आसक्ति भी पैदा कर लेते हैं, पर अपनी आत्मसत्ता से निस्सृत हो रही देववाणी नहीं सुन पाते । शिष्यत्व का एक प्रमुख लक्षण है-इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का त्याग । जिसने अपनी कामनाएँ छोड़ दीं, उसका मन-चित्त संयत हो गया और फिर वह परमात्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गया । गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं-च्च्कहऊँ कवन सिधि लोक रिझाए।ज्ज् तुम खुद सोचो कि लोक को रिझाकर कौन-सी सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी । फिर न जाने क्यों हम बार-बार उसी मार्ग पर चले जाते हैं। ऋषियों के अनुसार यही माया है ।
गीता के छठे अध्याय के इन दोनों श्लोकों-१८वें व १९वें का मर्म यही है कि ध्यान सफल तब ही होगा, जब हम कामनाओं के जाल से निकलेंगे । ध्यान अपने चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया भी है तथा उस ध्यान को कैसे किया जाए, इसके लिए श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे दैनंदिन जीवन का है-हमारी पूजास्थली में वायुरहित स्थान पर रखा एक दीपक, जिसकी ज्योति निरंतर प्रज्वलित है, निष्कंप है एवं हमें, हमारे चित्त को भी इस संसार-सागर में वैसा ही बनाए रखने की प्रेरणा देती है । हम कितने ही बुद्धिवादी हों, शास्त्रज्ञान जानते हों, यह स्पष्ट मान लें कि उससे आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं । बुद्घि के बंधनों-वासना, तृष्णा, अहंताओं से ऊपर जाकर ही हम शुद्ध आनंदमय चैतन्य को पा सकते हैं ।
Versions
-
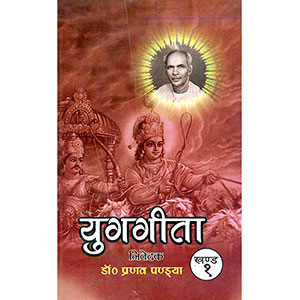
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
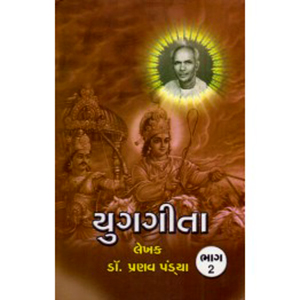
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
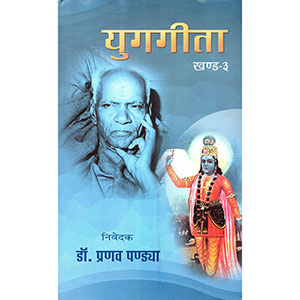
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
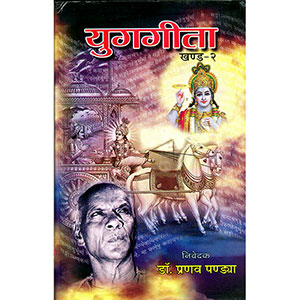
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
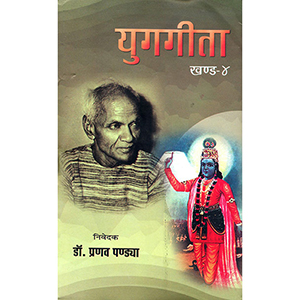
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
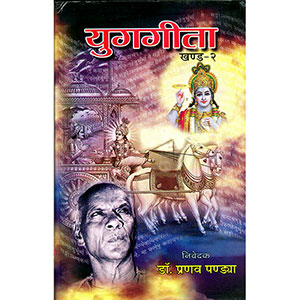
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
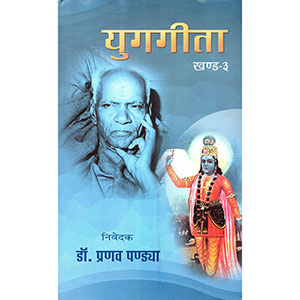
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
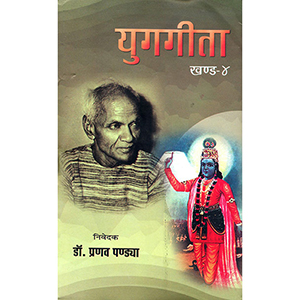
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
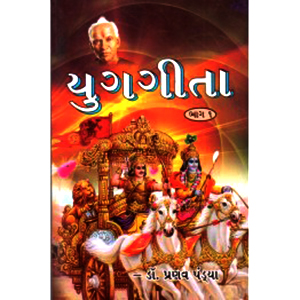
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- तृतीय खण्ड की प्रस्तावना
- प्रस्तुत चतुर्थ खण्ड की प्रस्तावना
- एकाकी यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः
- ध्यान हेतु व्यावहारिक निर्देश देते एक कुशल शिक्षक
- सबसे बड़ा अनुदान परमानंद की पराकाष्ठा वाली दिव्य शांति
- युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
- कैसा होना चाहिए योगी का संयत चित्त
- योग की चरमावस्था की ओर ले जाते योगेश्वर
- परमात्मारूपी लाभ को प्राप्त व्यक्ति दुःख में विचलित नहीं होता
- बार-बार मन को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाए
- चित्तवृत्ति निरोध एवं परमानन्द प्राप्ति का राजमाग
- ध्यान की पराकाष्ठा पर होती है सर्वोच्च अनुभूति
- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
- सुख या दुख में सर्वत्र समत्व के दर्शन करता है योगी
- कैसे आए यह चंचल मन काबू में?
- अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते
- कल्याणकारी कार्य करने वाले साधक की कभी दुर्गति नहीं होती
- भविष्य में हमारी क्या गति होगी, हम स्वयं निर्धारित करते हैं
- योग पथ पर चलने वाले का सदा कल्याण ही कल्याण है
- तस्मात् योगी भवार्जुन्
- वही ध्यानयोगी है श्रेष्ठ जो प्रभु को समर्पित है

