युगगीता (भाग-४) 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः
Read Scan Version
ध्यान में विघ्र क्या- क्या हैं ?
श्रीकृष्ण योग की महायात्रा पर अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं। इसके लिए उसे जितेंद्रिय (संयमी) होने, राग- द्वेष से परे चलने, मौसम आदि से प्रभावित न हो आत्मनिष्ठ बनने, मान- अपमान से परे चलकर ज्ञान- विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर निर्विकार ,, कूटस्थ व तृष्णामुक्त बनने तथा हर किसी के प्रति एकत्व भाव से जीने का संदेश दे रहे हैं। इतनी तैयारी किए बिना योग, जो सभी दुःखों का नाश कर देने वाला है, सध नहीं सकता। योगी के मन में किसी के भी प्रति एकांगी भाव नहीं होना चाहिए—चाहे वे पापी हों या धर्मात्मा, मित्र हों या शत्रु। ऐसी समत्व की दृष्टि रखने वाला ही योगी बन पाता है एवं अपनी मनोभूमि ऐसी बना पाता है कि वह ध्यान कर सके। इससे पूर्व वे दूसरे अध्याय में कह चुके हैं—‘‘समत्व योग उच्यते।’’ अर्थात् समभाव की दृष्टि का विकास। बिना इतने गुणों को विकसित किए साधक की मनोभूमि परिपक्व नहीं बन पाती। जैसे ही योगी ने, साधक ने यह जान लिया कि हम सभी नितांत शुद्ध एक ही आत्मा हैं, उस परमात्मारूपी महासूर्य की एक रश्मि हैं। तब हमारा अंतःकरण ध्यान की स्थिति में जाने को तैयार हो जाता है। ध्यान में सबसे बड़ा विघ्र है—ईर्ष्या, द्वेष का भाव, किसी के प्रति बैरभाव। जब तक अंदर से प्रेम की भाषा नहीं बोलने लगती, तब तक भावचेतना अंदर प्रवेश नहीं हो पाती। तृप्ति, तुष्टि, शांति मनुष्य को तब ही मिल सकती है, जब वह इन सभी उद्वेगों से परे चला जाए। है यह बहुत कठिन; किंतु ध्यानस्थ होना भी तो परमात्मा से मिलन है और यह मिलन इतना आसान भी नहीं होता।
श्री अरविंद को हुए योगेश्वर के दर्शन
श्री अरविंद स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जेल में थे। वहीं साधनारत श्री अरविंद को भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन हुए। अपने इस दर्शन व अनुभूति के विषय में श्री अरविंद ने उत्तरपाड़ा के भाषण में जनसाधारण को बताया तथा बाद में अपनी पत्रिका ‘वंदेमातरम्’ में प्रकाशित भी किया। भगवान् वासुदेव ने उनसे कहा, ‘‘तुम्हारे मन में बार- बार एक बात आ रही है और वह तुम्हारी ध्यान- साधना में विघ्र डाल रही है। वह है, हमें जेल में बंद क्यों किया गया? राष्ट्र के लिए किए गए एक श्रेष्ठ कर्म के लिए हमें बंद क्यों कर दिया गया और वह भी डाकू- हत्यारों करने वालों के बीच? हम तो निर्दोष थे, फिर यह दंड क्यों? क्या राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रयास करना इतना गलत कार्य है।’’ भगवान् ने उनसे फिर कहा, ‘‘हमने तुम्हें संदेश दिया था कि एकांत में जाओ, आत्मपर्यवेक्षण करो और अपने आप में स्थित हो जाओ, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने बम फोड़े, तरह- तरह के ऐसे काम किए, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे कार्यों में लगो। यद्यपि वे थे एक शुभ कार्य के निमित्त। मैं वासुदेव कृष्ण भी भारत को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ।
यदि मैं ऐसा चाहता हूँ तो इस पुण्यभूमि भारत को आजाद कराने से कौन रोक सकता है। तुम भी नहीं रोक सकते। तुम एक उच्चस्तरीय आत्मा हो। अतः एकांत में जाओ—अपने आपे का अध्ययन करो—इसलिए तुम्हें जेल में बंद करने का क्रम बना- तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ- कहाँ स्थित हूँ। तुम्हारे आस- पास बैठे सभी डकैतों- पापियों में मैं श्रीकृष्ण विराजमान हूँ।’’ श्री अरविंद ने दिव्यदृष्टि पाई व देखा कि सभी ओर जेल में, वार्डन में हर अपराधी में साक्षात् परमेश्वर, वासुदेव श्रीकृष्ण विद्यमान हैं। श्रीकृष्ण की छवि एक काली छाया के पीछे स्पष्ट दीख रही थी। श्रीकृष्ण बोले, ‘‘चित्तवृत्तियों के अंधकार के रूप में इनके ये पाप छिपे पड़े हैं। जिस दिन ये मिट जाएँगे, ये डकैत, पापी, अपराधी भी अपने अंदर के कृष्ण को पा लेंगे। तुम मानकर चलो, सभी में एक परमात्मा की सत्ता विराजमान है। धर्मात्मा व पापी, दोनों में एक भाव स्थापित करके चलो। समय आने पर तुम यहाँ से छूटोगे एवं एकांत साधना का अवसर तुम्हें मिलेगा। तब तुम्हें अनुभूति होगी कि यह जेलयात्रा कितने बड़े उद्देश्य के लिए थी।’’
समबुद्धि का भाव
भगवान् के श्री अरविंद को दिए गए इस उपदेश, उनकी इस अनुभूति का हम भली भाँति अध्ययन करें। सबके पीछे समभाव रखने की बात भगवान् कह रहे हैं। कभी भी कालिमा भरा आवरण हटा, तो रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, आम्रपाली साध्वी बन सकती है एवं बिल्वमंगल सूरदास बन सकता है। बस परदा हटने भर की देर है और अच्छे- खासे धर्मात्मा- पुण्यवाले के कर्म भी यदि गलत होने लगें, तो यह कालिमा भरा परदा छा सकता है। हम दोनों को समभाव से देखें, यह भगवान् का उपदेश है—साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिः। यही नहीं मित्र, हमसे बैर रखने वाले, हमारे शुभेच्छु (स्वार्थरहित भाव से सभी का हित चाहने वाले सुहृद) पक्षपातरहित भाव से हमसे जुड़े (उदासीन) दोनों ओर की भलाई चाहने वाले (मध्यस्थ) एवं द्वेषभाव रखने वाले बंधुगणों में भी हम समभाव रखें। किसी के प्रति पूर्वाग्रह न पालें। किसी की हमारे प्रति भिन्न प्रकार की भावना से हम प्रभावित न होकर उनके अंदर की ईश्वरीय सत्ता का मात्र दर्शन करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारे अंदर का योगी सतत जाग्रत् बना रह, अपने पुरुषार्थ में लगा रह, लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा।
श्री अरविंद को वासुदेव एक और महत्त्वपूर्ण संदेश दे चुके हैं—एकांत में रहने की बात। वही चर्चा अब योग की अगली कक्षा के अंतर्गत सटीक मार्गदर्शन दे रहे श्रीकृष्ण के श्रीमुख से दसवें श्लोक में निःसृत हो रहा है। क्या विलक्षण संयोग है। ध्यान रखने की बात है कि यह सारी चर्चा होने, ध्यान करने के पूर्व की चल रही है—
रहसि स्थितः
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥- ६/१०
पहले शब्दों के अर्थ से मूल आशय समझने का प्रयास करते हैं—
योगीपुरुष (योगी) एकांत में (रहसि) निरंतर (सततम्) अवस्थित होकर (स्थितः) शरीर एवं मन को नियंत्रित कर (यतचित्तात्मा) कामना रहित (निराशीः) किसी से कुछ ग्रहण न कर (अपरिग्रहः) अपने चित्त को—अंतःकारण को (आत्मानं) आत्मा में नियोजित रखते हैं (युञ्जीत)।
अब भावार्थ हुआ, ‘‘मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने नियंत्रण में रखने वाला, आशा और संग्रह- परिग्रह की वृत्ति से छुटकारा पा लेने वाला योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में नियोजित करता है अर्थात् उसे निरंतर इन साधनों द्वारा मन और बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए।’’
मनुष्य आज लौकिक जीवन के शोर- शराबों में उलझकर अपने अंतः के स्वरों को सुनना भूल गया है। वह बहिर्मुखी अधिक है। विज्ञान के चरम स्तर पर ले जाने वाले आविष्कारों ने भी उसके बहिर्मुखी बनने में मदद की है। बहिर्मुखी स्वभाव वाला चंचल चित्त जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, बार- बार भागता है, उन्हीं में रमण करता है, जहाँ उसे तात्कालिक आकर्षण नजर आता है। दुनिया भर की आकांक्षाएँ, महत्त्वाकांक्षाएँ वह पाल लेता है। ढेर सारे साधनों का जखीरा खड़ा कर लेता है। कभी- कभी काम आने वाले, कभी भी काम में न आने वाले ढेरों संसाधन रखकर वह सोचता है कि उसके सुख की प्राप्ति में ये सभी मदद करेंगे, पर ऐसा होता नहीं। मन व इंद्रियाँ नियंत्रित होती नहीं, तृष्णा की अग्रि सतत जलती रहती है, जितना इसमें डालो, उतनी ही बढ़ती चली जाती है, फिर योग कैसे सधे? योगस्थ हो ध्यान कैसे लगे? मन एकाग्र किस प्रकार हो। यदि एकांत में गए भी तो वहाँ नियमन संयम के अभाव में, परिग्रह की वृत्ति के कारण एकाग्रता सधेगी नहीं। हम एकांत में न रहकर अपनी आशाओं, इच्छाओं, मनोकामनाओं के साथ जी रहे होंगे। स्थूल दृष्टि से हम एकांत में हो सकते हैं, पर मन हमारा ढेरों साथियों के साथ वहाँ बैठा हमारी साधना में विघ्र बना हुआ है। ऐसे में एकांत साधना मजाक ही बनकर रह जाती है।
एकांत साधना का मर्म
अनेक व्यक्ति मौन साधना, एकांत साधना, गुफा में ध्यान, हिमालय में एकाकी रहने के भाव से प्रयासरत होते हैं, पर यदि उनने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रित नहीं किया है, ढेर सारी कामनाएँ मन में लिए बैठे हैं, साधनों की कामना भी है, वे साथ में हैं भी और कोई और दे जाए तथा संग्रह करने की वृत्ति भी जिंदा है, तो वह साधना सधेगी नहीं। शान्तिकुञ्ज हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में १९७३ में एकांत में प्राण- प्रत्यावर्तन साधना सत्र (५ दिवसीय) संपन्न हुए। उन सबका एक ही उद्देश्य था—एकांत में अपने आपे से साक्षात्कार एवं आत्मा को परमात्मा में स्थित करने की योग- साधना। इसके लिए प्रातः से सायं तक ढेरों साधनाएँ कराई जाती थीं। परमपूज्य गुरुदेव के चौबीस लक्ष के गायत्री जपरूपी तप एवं उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के संरक्षण में कइयों ने वह साध भी लिया। प्राणऊर्जा भी वे पूज्यवर से पा सके, परंतु जो मन को खाली न कर पाए, उनके वे पाँच दिन निकल गए। हाथ में आया एक सौभाग्य वापस चला गया। पिछले दिनों विगत तीन वर्षों से शान्तिकुञ्ज हरिद्वार में पुनः एकांत के मौन अंतः ऊर्जा जागरण सत्रों की शृंखला चली है। इसमें भी वे साधनाएँ कराई जाती हैं तथा अपने आपे से साक्षात्कार का अभ्यास किया जाता है। इस एकांत साधना में वे पाँच दिन मौन रहते हैं, निर्धारित आहार लेते हैं, नियमित स्वाध्याय करते हैं एवं निर्देशों के अनुसार अपने कक्ष में एकाकी विभिन्न साधनाएँ करते रहते हैं। सभी वे लाभ नहीं ले पाते, जो किसी मन के बैरागी को, अपनी सभी इच्छाएँ गुरुचरणों में सौंपकर निष्काम भाव से साधना करने वालों को मिलते हैं। साधनाएँ सभी फल देती हैं, पर ध्यानस्थ स्थिति में जाने से पूर्व की तैयारियाँ तो हों। यदि पूर्व तैयारी नहीं है तो मन (अंतःकरण) वैसा ही रहेगा, भले ही कक्ष में बंद हो, जैसा पहले बाहर था। इसीलिए इतनी उच्चस्तरीय साधना के मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाते। पात्रता का अर्जन सबसे पहली आवश्यकता है। क्या हैं वे शर्तें, जो प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं।
ध्यानस्थ होने की पूर्व शर्तें
(१) एकांत में निरंतर अकेले स्थित रहना (२) शरीर और मन को इंद्रियों सहित नियंत्रण में रखना (३) किसी भी प्रकार की कामना- आशा मन में न रखना (४) अपरिग्रह की वृत्ति विकसित कर न्यूनतम साधनों में कार्य चलाना, अपनी ब्राह्मणोचित वृत्ति को जिंदा बनाए रखना एवं (५) निरंतर मन और बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास करते रहना।
पाँचों शर्तें जरूरी हैं—ध्यानस्थ स्थिति में जाकर अपनी आत्मसत्ता को परमात्मसत्ता में नियोजित करने के लिए, परमशांति की प्राप्ति के लिए तथा परमलक्ष्य को पाने हेतु। यह श्रीकृष्ण का, आत्मोन्नति, के पथ पर जाने वाले हर साधक के लिए खुला आमंत्रण है। बार- बार द्वितीय अध्याय के बाद वे कहते चले जा रहे हैं कि मन- बुद्धि द्वारा एकाग्रता सर्वाधिक अनिवार्य है। ‘‘वशे हि यस्य इंद्रियाणि’’ से लेकर यहाँ ‘‘योगी युञ्जीत सततमात्मानं’’ तक वही संबोधन है। यहाँ भी वे एकांतसेवन के साथ यही शर्त जोड़ रहे हैं। यदि इंद्रियाँ नियंत्रण में नहीं हैं तो एकांत सेवन करने वाला साधक स्थूल दृष्टि से भले ही अकेला रह रहा हो, उसका मन कहीं और रमण कर रहा होगा। फिर योग सधे कैसे? इसी तरह श्रीकृष्ण अपरिग्रही होने एवं निष्काम भाव से कर्म करने की बात कहते हैं। परिग्रह एवं कामनाएँ ही समस्त दुःखों के हेतु हैं। अधिक- से पाने की कामना, संग्रह करने की इच्छा, आध्यात्मिक अनुशासनों के विपरीत जाती है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, बनने का स्वाँग भर कर सकता है।
हर शब्द में छिपा है मर्म
यहाँ ‘अपरिग्रह’ से यह आशय भी योगेश्वर श्रीकृष्ण का है कि यदि हम योगी बनना चाह रहे हैं तो किसी से कुछ ग्रहण न कर अपने मन पर अपना नियंत्रण रखें। जब हमारे अंदर लेने की कामना जागती है तो हमारी रुचि अनावश्यक संग्रह की ओर बढ़ने लगती है। निराशीः अपरिग्रहः के माध्यम से अर्जुन को यही संकेत किया गया है कि किसी से कुछ आशा न रखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, मनोकामनाओं को मत पालो एवं साधनों को भी स्वीकार करने की वृत्ति से दूर रहो। यह अपरिग्रह मानसिक गुण ज्यादा है। यह जब स्वभाव में आ जाता है तो मन इतना प्रचंड, समर्थ एवं सशक्त हो जाता है कि न्यूनतम में निर्वाह करने में सतत संतुष्ट रहता है। यही निर्देश सतत अंदर से निर्णायक बुद्धि को जाता है कि लौकिक साधनों के संग्रह से, उन्हें औरों से स्वीकार करने से दूर रहो, अनावश्यक महत्त्वाकांक्षाएँ मत पालो।
यह श्लोक अपने विलक्षण अर्थ के साथ किसी योगी के लिए तो महत्त्वपूर्ण है ही, एक आदर्श कार्यकर्त्ता, युगनिर्माण जैसे महती प्रयोजन में जुटे देवमानव के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। भले ही युगनिर्माण जैसे कार्य में एकाकी रहना उचित न माना जाए, पर यहाँ रहसि स्थितः एकांत में स्थित होने की जो बात कही है, वह एकांत की मनःस्थिति की बात है। जग के कोलाहल में भी जो मस्ती से रहकर साधनात्मक पुरुषार्थ करता है, लोकमंगल के लिए जीता है, वह प्रकारांतर से योगी ही कहलाता है। हम भी एक आदर्श साधक बनें, योग में स्थित होकर कर्म करें, यह अपेक्षा योगेश्वर श्रीकृष्ण की है।
सांसारिक विषयों से, साधनों के संचय से मनुष्य की तृप्ति संभव नहीं है। ये क्षणिक सुख अंततः दुःख का कारण ही बनते हैं। जैसे ही हम अपने आसपास की सांसारिक परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लेते हैं, हमारी प्रसन्नता का आंतरिक स्रोत फूट पड़ता है। अभिमान और कामोद्वेगों के विकारों में उलझा मनुष्य तो सतत इस संसार में भटकता ही रहता है। अपने आपे से अलगाव को दूर करने के लिए ध्यान करने की अनिवार्यता है। यह हमें अपने आप से मिलता है। आत्मसाक्षात्कार कराता है। बहिर्मुखी मन द्वारा किसी भी स्थिति में ध्यान संभव नहीं है, यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए।
चलें, अब व्यवहार की ओर
भगवान् सिद्धांत समझाते- समझाते अब व्यावहारिक प्रयोगों पर क्रमशः आ गए हैं। योग कैसे करें? कैसे योग में स्थित हों? कैसे ध्यान की गहराइयों में डुबकियाँ लगाएँ? यह हर साधक की जिज्ञासा है। योग एवं ध्यान क्रिया नहीं है। ऐसी ‘टास्क’ नहीं हैं, जिन्हें किया जाता है। ध्यान के लिए कहीं- कहीं उपयुक्त वातावरण भी मिलता है एवं मनःस्थिति की यदि उसके साथ सही ट्यूनिंग हो जाए, दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, तो ध्यान स्वतः लग जाता है। मनःस्थिति बनाने की प्रक्रिया की व्यावहारिक व्याख्या यहाँ दसवें श्लोक में है और फिर अगले श्लोकों में वह चर्चा है, उसमें कहाँ बैठा जाए, कैसे बैठा जाए, यह बताया गया है।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥ ६/११
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः।
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म्विशुद्धये॥ ६/१२
शुद्धस्थान में (शुचौ) स्थिर भाव से (स्थिरं) जो अति ऊँचा नहीं है (न अति उच्छ्रितं) न ही अत्यधिक नीचा (न अति नीचं) कुश- तृण बिछाकर उस पर मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर (चैल- अजिन उत्तरम्) अपना (आत्मनः) आसन (आसनम्) स्थापित करके (प्रतिष्ठाप्य) उस (तत्र) आसन पर (आसने) बैठकर (उपविश्य) चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए (यत चित्त- इंद्रियक्रियाः) मन को (मनः) एकाग्र- आत्मपरायण करके (एकाग्रं कृत्वा) अंतःकरण की शुद्धि के लिए (आत्मविशुद्धये) जीवात्मा और परमात्मा की एकता की भावना में तन्मय होकर योगस्थ होकर (योगं) योग का अभ्यास करे (युञ्ज्यात्)।
पूरे का भावार्थ हुआ—शुद्ध पवित्र स्थान में अपना आसन लगाकर जो न बहुत ऊँचा हो, न ही नीचा हो और जिसमें कुशा, मृगछाला और वस्त्र क्रमशः बिछे हों, ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके साधक को अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। ६/११, १२
स्पष्टतः ध्यान के आसन संबंधी निर्देश श्रीकृष्ण ने यहाँ दिए हैं। स्थान स्वच्छ हो, स्थिर आसन हो। न स्प्रिंग हो, न फोम के गद्दे। फर्श की सीलन से बचने के लिए सूखी घास- तृण हो, उस पर मृगछाला और उस पर एक सूती कपड़ा। न यह ऊँचा हो, न नीचा। ऐसा हुआ तो मन एकाग्र होगा। खूब हवादार स्थान हो। ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके (तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा) चित्त की क्रियाओं को संयत कर हृदय की, अंतःकरण की शुद्धि का अभ्यास करो। यह ध्यान की तैयारी है।
श्रीकृष्ण योग की महायात्रा पर अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं। इसके लिए उसे जितेंद्रिय (संयमी) होने, राग- द्वेष से परे चलने, मौसम आदि से प्रभावित न हो आत्मनिष्ठ बनने, मान- अपमान से परे चलकर ज्ञान- विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर निर्विकार ,, कूटस्थ व तृष्णामुक्त बनने तथा हर किसी के प्रति एकत्व भाव से जीने का संदेश दे रहे हैं। इतनी तैयारी किए बिना योग, जो सभी दुःखों का नाश कर देने वाला है, सध नहीं सकता। योगी के मन में किसी के भी प्रति एकांगी भाव नहीं होना चाहिए—चाहे वे पापी हों या धर्मात्मा, मित्र हों या शत्रु। ऐसी समत्व की दृष्टि रखने वाला ही योगी बन पाता है एवं अपनी मनोभूमि ऐसी बना पाता है कि वह ध्यान कर सके। इससे पूर्व वे दूसरे अध्याय में कह चुके हैं—‘‘समत्व योग उच्यते।’’ अर्थात् समभाव की दृष्टि का विकास। बिना इतने गुणों को विकसित किए साधक की मनोभूमि परिपक्व नहीं बन पाती। जैसे ही योगी ने, साधक ने यह जान लिया कि हम सभी नितांत शुद्ध एक ही आत्मा हैं, उस परमात्मारूपी महासूर्य की एक रश्मि हैं। तब हमारा अंतःकरण ध्यान की स्थिति में जाने को तैयार हो जाता है। ध्यान में सबसे बड़ा विघ्र है—ईर्ष्या, द्वेष का भाव, किसी के प्रति बैरभाव। जब तक अंदर से प्रेम की भाषा नहीं बोलने लगती, तब तक भावचेतना अंदर प्रवेश नहीं हो पाती। तृप्ति, तुष्टि, शांति मनुष्य को तब ही मिल सकती है, जब वह इन सभी उद्वेगों से परे चला जाए। है यह बहुत कठिन; किंतु ध्यानस्थ होना भी तो परमात्मा से मिलन है और यह मिलन इतना आसान भी नहीं होता।
श्री अरविंद को हुए योगेश्वर के दर्शन
श्री अरविंद स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जेल में थे। वहीं साधनारत श्री अरविंद को भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन हुए। अपने इस दर्शन व अनुभूति के विषय में श्री अरविंद ने उत्तरपाड़ा के भाषण में जनसाधारण को बताया तथा बाद में अपनी पत्रिका ‘वंदेमातरम्’ में प्रकाशित भी किया। भगवान् वासुदेव ने उनसे कहा, ‘‘तुम्हारे मन में बार- बार एक बात आ रही है और वह तुम्हारी ध्यान- साधना में विघ्र डाल रही है। वह है, हमें जेल में बंद क्यों किया गया? राष्ट्र के लिए किए गए एक श्रेष्ठ कर्म के लिए हमें बंद क्यों कर दिया गया और वह भी डाकू- हत्यारों करने वालों के बीच? हम तो निर्दोष थे, फिर यह दंड क्यों? क्या राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रयास करना इतना गलत कार्य है।’’ भगवान् ने उनसे फिर कहा, ‘‘हमने तुम्हें संदेश दिया था कि एकांत में जाओ, आत्मपर्यवेक्षण करो और अपने आप में स्थित हो जाओ, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने बम फोड़े, तरह- तरह के ऐसे काम किए, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे कार्यों में लगो। यद्यपि वे थे एक शुभ कार्य के निमित्त। मैं वासुदेव कृष्ण भी भारत को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ।
यदि मैं ऐसा चाहता हूँ तो इस पुण्यभूमि भारत को आजाद कराने से कौन रोक सकता है। तुम भी नहीं रोक सकते। तुम एक उच्चस्तरीय आत्मा हो। अतः एकांत में जाओ—अपने आपे का अध्ययन करो—इसलिए तुम्हें जेल में बंद करने का क्रम बना- तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ- कहाँ स्थित हूँ। तुम्हारे आस- पास बैठे सभी डकैतों- पापियों में मैं श्रीकृष्ण विराजमान हूँ।’’ श्री अरविंद ने दिव्यदृष्टि पाई व देखा कि सभी ओर जेल में, वार्डन में हर अपराधी में साक्षात् परमेश्वर, वासुदेव श्रीकृष्ण विद्यमान हैं। श्रीकृष्ण की छवि एक काली छाया के पीछे स्पष्ट दीख रही थी। श्रीकृष्ण बोले, ‘‘चित्तवृत्तियों के अंधकार के रूप में इनके ये पाप छिपे पड़े हैं। जिस दिन ये मिट जाएँगे, ये डकैत, पापी, अपराधी भी अपने अंदर के कृष्ण को पा लेंगे। तुम मानकर चलो, सभी में एक परमात्मा की सत्ता विराजमान है। धर्मात्मा व पापी, दोनों में एक भाव स्थापित करके चलो। समय आने पर तुम यहाँ से छूटोगे एवं एकांत साधना का अवसर तुम्हें मिलेगा। तब तुम्हें अनुभूति होगी कि यह जेलयात्रा कितने बड़े उद्देश्य के लिए थी।’’
समबुद्धि का भाव
भगवान् के श्री अरविंद को दिए गए इस उपदेश, उनकी इस अनुभूति का हम भली भाँति अध्ययन करें। सबके पीछे समभाव रखने की बात भगवान् कह रहे हैं। कभी भी कालिमा भरा आवरण हटा, तो रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, आम्रपाली साध्वी बन सकती है एवं बिल्वमंगल सूरदास बन सकता है। बस परदा हटने भर की देर है और अच्छे- खासे धर्मात्मा- पुण्यवाले के कर्म भी यदि गलत होने लगें, तो यह कालिमा भरा परदा छा सकता है। हम दोनों को समभाव से देखें, यह भगवान् का उपदेश है—साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिः। यही नहीं मित्र, हमसे बैर रखने वाले, हमारे शुभेच्छु (स्वार्थरहित भाव से सभी का हित चाहने वाले सुहृद) पक्षपातरहित भाव से हमसे जुड़े (उदासीन) दोनों ओर की भलाई चाहने वाले (मध्यस्थ) एवं द्वेषभाव रखने वाले बंधुगणों में भी हम समभाव रखें। किसी के प्रति पूर्वाग्रह न पालें। किसी की हमारे प्रति भिन्न प्रकार की भावना से हम प्रभावित न होकर उनके अंदर की ईश्वरीय सत्ता का मात्र दर्शन करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारे अंदर का योगी सतत जाग्रत् बना रह, अपने पुरुषार्थ में लगा रह, लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा।
श्री अरविंद को वासुदेव एक और महत्त्वपूर्ण संदेश दे चुके हैं—एकांत में रहने की बात। वही चर्चा अब योग की अगली कक्षा के अंतर्गत सटीक मार्गदर्शन दे रहे श्रीकृष्ण के श्रीमुख से दसवें श्लोक में निःसृत हो रहा है। क्या विलक्षण संयोग है। ध्यान रखने की बात है कि यह सारी चर्चा होने, ध्यान करने के पूर्व की चल रही है—
रहसि स्थितः
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥- ६/१०
पहले शब्दों के अर्थ से मूल आशय समझने का प्रयास करते हैं—
योगीपुरुष (योगी) एकांत में (रहसि) निरंतर (सततम्) अवस्थित होकर (स्थितः) शरीर एवं मन को नियंत्रित कर (यतचित्तात्मा) कामना रहित (निराशीः) किसी से कुछ ग्रहण न कर (अपरिग्रहः) अपने चित्त को—अंतःकारण को (आत्मानं) आत्मा में नियोजित रखते हैं (युञ्जीत)।
अब भावार्थ हुआ, ‘‘मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने नियंत्रण में रखने वाला, आशा और संग्रह- परिग्रह की वृत्ति से छुटकारा पा लेने वाला योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में नियोजित करता है अर्थात् उसे निरंतर इन साधनों द्वारा मन और बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए।’’
मनुष्य आज लौकिक जीवन के शोर- शराबों में उलझकर अपने अंतः के स्वरों को सुनना भूल गया है। वह बहिर्मुखी अधिक है। विज्ञान के चरम स्तर पर ले जाने वाले आविष्कारों ने भी उसके बहिर्मुखी बनने में मदद की है। बहिर्मुखी स्वभाव वाला चंचल चित्त जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, बार- बार भागता है, उन्हीं में रमण करता है, जहाँ उसे तात्कालिक आकर्षण नजर आता है। दुनिया भर की आकांक्षाएँ, महत्त्वाकांक्षाएँ वह पाल लेता है। ढेर सारे साधनों का जखीरा खड़ा कर लेता है। कभी- कभी काम आने वाले, कभी भी काम में न आने वाले ढेरों संसाधन रखकर वह सोचता है कि उसके सुख की प्राप्ति में ये सभी मदद करेंगे, पर ऐसा होता नहीं। मन व इंद्रियाँ नियंत्रित होती नहीं, तृष्णा की अग्रि सतत जलती रहती है, जितना इसमें डालो, उतनी ही बढ़ती चली जाती है, फिर योग कैसे सधे? योगस्थ हो ध्यान कैसे लगे? मन एकाग्र किस प्रकार हो। यदि एकांत में गए भी तो वहाँ नियमन संयम के अभाव में, परिग्रह की वृत्ति के कारण एकाग्रता सधेगी नहीं। हम एकांत में न रहकर अपनी आशाओं, इच्छाओं, मनोकामनाओं के साथ जी रहे होंगे। स्थूल दृष्टि से हम एकांत में हो सकते हैं, पर मन हमारा ढेरों साथियों के साथ वहाँ बैठा हमारी साधना में विघ्र बना हुआ है। ऐसे में एकांत साधना मजाक ही बनकर रह जाती है।
एकांत साधना का मर्म
अनेक व्यक्ति मौन साधना, एकांत साधना, गुफा में ध्यान, हिमालय में एकाकी रहने के भाव से प्रयासरत होते हैं, पर यदि उनने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रित नहीं किया है, ढेर सारी कामनाएँ मन में लिए बैठे हैं, साधनों की कामना भी है, वे साथ में हैं भी और कोई और दे जाए तथा संग्रह करने की वृत्ति भी जिंदा है, तो वह साधना सधेगी नहीं। शान्तिकुञ्ज हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में १९७३ में एकांत में प्राण- प्रत्यावर्तन साधना सत्र (५ दिवसीय) संपन्न हुए। उन सबका एक ही उद्देश्य था—एकांत में अपने आपे से साक्षात्कार एवं आत्मा को परमात्मा में स्थित करने की योग- साधना। इसके लिए प्रातः से सायं तक ढेरों साधनाएँ कराई जाती थीं। परमपूज्य गुरुदेव के चौबीस लक्ष के गायत्री जपरूपी तप एवं उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के संरक्षण में कइयों ने वह साध भी लिया। प्राणऊर्जा भी वे पूज्यवर से पा सके, परंतु जो मन को खाली न कर पाए, उनके वे पाँच दिन निकल गए। हाथ में आया एक सौभाग्य वापस चला गया। पिछले दिनों विगत तीन वर्षों से शान्तिकुञ्ज हरिद्वार में पुनः एकांत के मौन अंतः ऊर्जा जागरण सत्रों की शृंखला चली है। इसमें भी वे साधनाएँ कराई जाती हैं तथा अपने आपे से साक्षात्कार का अभ्यास किया जाता है। इस एकांत साधना में वे पाँच दिन मौन रहते हैं, निर्धारित आहार लेते हैं, नियमित स्वाध्याय करते हैं एवं निर्देशों के अनुसार अपने कक्ष में एकाकी विभिन्न साधनाएँ करते रहते हैं। सभी वे लाभ नहीं ले पाते, जो किसी मन के बैरागी को, अपनी सभी इच्छाएँ गुरुचरणों में सौंपकर निष्काम भाव से साधना करने वालों को मिलते हैं। साधनाएँ सभी फल देती हैं, पर ध्यानस्थ स्थिति में जाने से पूर्व की तैयारियाँ तो हों। यदि पूर्व तैयारी नहीं है तो मन (अंतःकरण) वैसा ही रहेगा, भले ही कक्ष में बंद हो, जैसा पहले बाहर था। इसीलिए इतनी उच्चस्तरीय साधना के मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाते। पात्रता का अर्जन सबसे पहली आवश्यकता है। क्या हैं वे शर्तें, जो प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं।
ध्यानस्थ होने की पूर्व शर्तें
(१) एकांत में निरंतर अकेले स्थित रहना (२) शरीर और मन को इंद्रियों सहित नियंत्रण में रखना (३) किसी भी प्रकार की कामना- आशा मन में न रखना (४) अपरिग्रह की वृत्ति विकसित कर न्यूनतम साधनों में कार्य चलाना, अपनी ब्राह्मणोचित वृत्ति को जिंदा बनाए रखना एवं (५) निरंतर मन और बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास करते रहना।
पाँचों शर्तें जरूरी हैं—ध्यानस्थ स्थिति में जाकर अपनी आत्मसत्ता को परमात्मसत्ता में नियोजित करने के लिए, परमशांति की प्राप्ति के लिए तथा परमलक्ष्य को पाने हेतु। यह श्रीकृष्ण का, आत्मोन्नति, के पथ पर जाने वाले हर साधक के लिए खुला आमंत्रण है। बार- बार द्वितीय अध्याय के बाद वे कहते चले जा रहे हैं कि मन- बुद्धि द्वारा एकाग्रता सर्वाधिक अनिवार्य है। ‘‘वशे हि यस्य इंद्रियाणि’’ से लेकर यहाँ ‘‘योगी युञ्जीत सततमात्मानं’’ तक वही संबोधन है। यहाँ भी वे एकांतसेवन के साथ यही शर्त जोड़ रहे हैं। यदि इंद्रियाँ नियंत्रण में नहीं हैं तो एकांत सेवन करने वाला साधक स्थूल दृष्टि से भले ही अकेला रह रहा हो, उसका मन कहीं और रमण कर रहा होगा। फिर योग सधे कैसे? इसी तरह श्रीकृष्ण अपरिग्रही होने एवं निष्काम भाव से कर्म करने की बात कहते हैं। परिग्रह एवं कामनाएँ ही समस्त दुःखों के हेतु हैं। अधिक- से पाने की कामना, संग्रह करने की इच्छा, आध्यात्मिक अनुशासनों के विपरीत जाती है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, बनने का स्वाँग भर कर सकता है।
हर शब्द में छिपा है मर्म
यहाँ ‘अपरिग्रह’ से यह आशय भी योगेश्वर श्रीकृष्ण का है कि यदि हम योगी बनना चाह रहे हैं तो किसी से कुछ ग्रहण न कर अपने मन पर अपना नियंत्रण रखें। जब हमारे अंदर लेने की कामना जागती है तो हमारी रुचि अनावश्यक संग्रह की ओर बढ़ने लगती है। निराशीः अपरिग्रहः के माध्यम से अर्जुन को यही संकेत किया गया है कि किसी से कुछ आशा न रखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, मनोकामनाओं को मत पालो एवं साधनों को भी स्वीकार करने की वृत्ति से दूर रहो। यह अपरिग्रह मानसिक गुण ज्यादा है। यह जब स्वभाव में आ जाता है तो मन इतना प्रचंड, समर्थ एवं सशक्त हो जाता है कि न्यूनतम में निर्वाह करने में सतत संतुष्ट रहता है। यही निर्देश सतत अंदर से निर्णायक बुद्धि को जाता है कि लौकिक साधनों के संग्रह से, उन्हें औरों से स्वीकार करने से दूर रहो, अनावश्यक महत्त्वाकांक्षाएँ मत पालो।
यह श्लोक अपने विलक्षण अर्थ के साथ किसी योगी के लिए तो महत्त्वपूर्ण है ही, एक आदर्श कार्यकर्त्ता, युगनिर्माण जैसे महती प्रयोजन में जुटे देवमानव के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। भले ही युगनिर्माण जैसे कार्य में एकाकी रहना उचित न माना जाए, पर यहाँ रहसि स्थितः एकांत में स्थित होने की जो बात कही है, वह एकांत की मनःस्थिति की बात है। जग के कोलाहल में भी जो मस्ती से रहकर साधनात्मक पुरुषार्थ करता है, लोकमंगल के लिए जीता है, वह प्रकारांतर से योगी ही कहलाता है। हम भी एक आदर्श साधक बनें, योग में स्थित होकर कर्म करें, यह अपेक्षा योगेश्वर श्रीकृष्ण की है।
सांसारिक विषयों से, साधनों के संचय से मनुष्य की तृप्ति संभव नहीं है। ये क्षणिक सुख अंततः दुःख का कारण ही बनते हैं। जैसे ही हम अपने आसपास की सांसारिक परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लेते हैं, हमारी प्रसन्नता का आंतरिक स्रोत फूट पड़ता है। अभिमान और कामोद्वेगों के विकारों में उलझा मनुष्य तो सतत इस संसार में भटकता ही रहता है। अपने आपे से अलगाव को दूर करने के लिए ध्यान करने की अनिवार्यता है। यह हमें अपने आप से मिलता है। आत्मसाक्षात्कार कराता है। बहिर्मुखी मन द्वारा किसी भी स्थिति में ध्यान संभव नहीं है, यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए।
चलें, अब व्यवहार की ओर
भगवान् सिद्धांत समझाते- समझाते अब व्यावहारिक प्रयोगों पर क्रमशः आ गए हैं। योग कैसे करें? कैसे योग में स्थित हों? कैसे ध्यान की गहराइयों में डुबकियाँ लगाएँ? यह हर साधक की जिज्ञासा है। योग एवं ध्यान क्रिया नहीं है। ऐसी ‘टास्क’ नहीं हैं, जिन्हें किया जाता है। ध्यान के लिए कहीं- कहीं उपयुक्त वातावरण भी मिलता है एवं मनःस्थिति की यदि उसके साथ सही ट्यूनिंग हो जाए, दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, तो ध्यान स्वतः लग जाता है। मनःस्थिति बनाने की प्रक्रिया की व्यावहारिक व्याख्या यहाँ दसवें श्लोक में है और फिर अगले श्लोकों में वह चर्चा है, उसमें कहाँ बैठा जाए, कैसे बैठा जाए, यह बताया गया है।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥ ६/११
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः।
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म्विशुद्धये॥ ६/१२
शुद्धस्थान में (शुचौ) स्थिर भाव से (स्थिरं) जो अति ऊँचा नहीं है (न अति उच्छ्रितं) न ही अत्यधिक नीचा (न अति नीचं) कुश- तृण बिछाकर उस पर मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर (चैल- अजिन उत्तरम्) अपना (आत्मनः) आसन (आसनम्) स्थापित करके (प्रतिष्ठाप्य) उस (तत्र) आसन पर (आसने) बैठकर (उपविश्य) चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए (यत चित्त- इंद्रियक्रियाः) मन को (मनः) एकाग्र- आत्मपरायण करके (एकाग्रं कृत्वा) अंतःकरण की शुद्धि के लिए (आत्मविशुद्धये) जीवात्मा और परमात्मा की एकता की भावना में तन्मय होकर योगस्थ होकर (योगं) योग का अभ्यास करे (युञ्ज्यात्)।
पूरे का भावार्थ हुआ—शुद्ध पवित्र स्थान में अपना आसन लगाकर जो न बहुत ऊँचा हो, न ही नीचा हो और जिसमें कुशा, मृगछाला और वस्त्र क्रमशः बिछे हों, ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके साधक को अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। ६/११, १२
स्पष्टतः ध्यान के आसन संबंधी निर्देश श्रीकृष्ण ने यहाँ दिए हैं। स्थान स्वच्छ हो, स्थिर आसन हो। न स्प्रिंग हो, न फोम के गद्दे। फर्श की सीलन से बचने के लिए सूखी घास- तृण हो, उस पर मृगछाला और उस पर एक सूती कपड़ा। न यह ऊँचा हो, न नीचा। ऐसा हुआ तो मन एकाग्र होगा। खूब हवादार स्थान हो। ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके (तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा) चित्त की क्रियाओं को संयत कर हृदय की, अंतःकरण की शुद्धि का अभ्यास करो। यह ध्यान की तैयारी है।
Versions
-
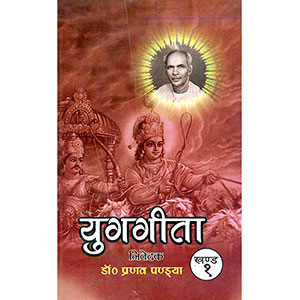
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
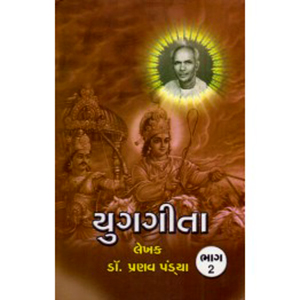
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
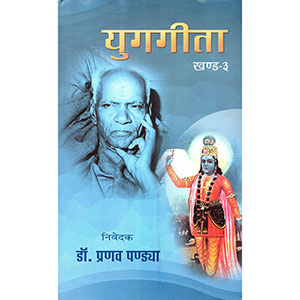
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
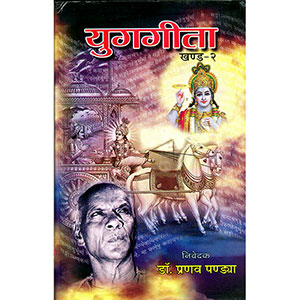
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
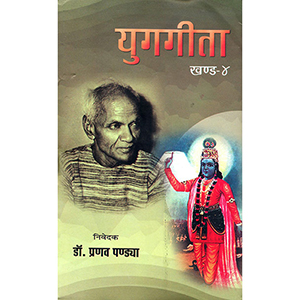
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
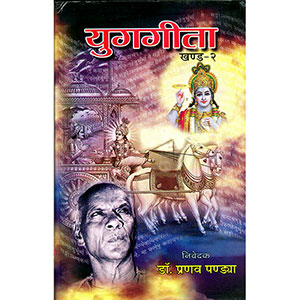
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
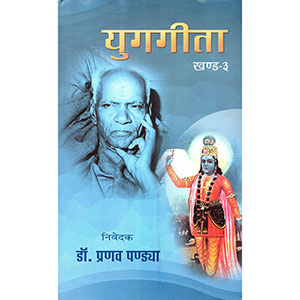
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
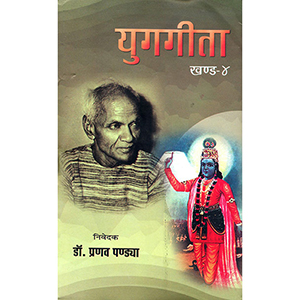
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
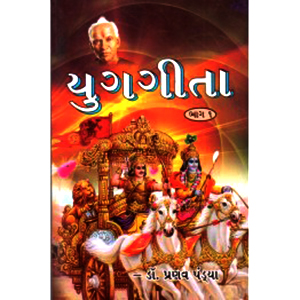
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- तृतीय खण्ड की प्रस्तावना
- प्रस्तुत चतुर्थ खण्ड की प्रस्तावना
- एकाकी यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः
- ध्यान हेतु व्यावहारिक निर्देश देते एक कुशल शिक्षक
- सबसे बड़ा अनुदान परमानंद की पराकाष्ठा वाली दिव्य शांति
- युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
- कैसा होना चाहिए योगी का संयत चित्त
- योग की चरमावस्था की ओर ले जाते योगेश्वर
- परमात्मारूपी लाभ को प्राप्त व्यक्ति दुःख में विचलित नहीं होता
- बार-बार मन को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाए
- चित्तवृत्ति निरोध एवं परमानन्द प्राप्ति का राजमाग
- ध्यान की पराकाष्ठा पर होती है सर्वोच्च अनुभूति
- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
- सुख या दुख में सर्वत्र समत्व के दर्शन करता है योगी
- कैसे आए यह चंचल मन काबू में?
- अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते
- कल्याणकारी कार्य करने वाले साधक की कभी दुर्गति नहीं होती
- भविष्य में हमारी क्या गति होगी, हम स्वयं निर्धारित करते हैं
- योग पथ पर चलने वाले का सदा कल्याण ही कल्याण है
- तस्मात् योगी भवार्जुन्
- वही ध्यानयोगी है श्रेष्ठ जो प्रभु को समर्पित है

