युगगीता (भाग-४) 
ध्यान की पराकाष्ठा पर होती है सर्वोच्च अनुभूति
Read Scan Version
विगत व्याख्या में इस अध्याय के छब्बीसवें श्लोक की विस्तृत विवेचना एवं सत्ताइसवें श्लोक
का अर्थ- शब्दार्थ भावार्थ बताया गया था। भगवान का स्पष्ट
निर्देश है कि हम मन को जब भी वह बार बार भटकता है- वहाँ से
उसे हटाकर आदर्शों के समुच्चय परमात्मा में ही नियोजित करें।
परमात्मा अर्थात आदर्शों का समूह। पतंजलि द्वारा मन की चंचलता का
स्वरूप- उसके कारण व उसका समाधान भी विगत अंक में बताए गए थे।
प्रभु की जीवन लीला में सतत चिंतन- मनन कभी मन को भटकने नहीं
देता। इसीलिये प्रयास यही हो कि हम चंचल चित्त को रोकें और
प्रभु में लगायें। यदि ऐसा हो गया तो ऐसा योगी जिसका मन भली
प्रकार शान्त है, जिसका रजोगुण दूर हो गया है तथा जिसने सभी
प्रकार के पापों से पल्ला छुड़ा लिया है- उसे सच्चिदानंदघन परमात्मा के साथ एकीभाव प्राप्त हो परमानंद की उपलब्धि होती है (श्लोक २७)। चार शर्त्ते भगवान ने रखी हैं। मन को विषयों से भटकने से रोककर उसे शान्त करना, रजोगुण कमकर सतोगुण बढ़ाना, ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति एवं वासनामुक्त पवित्र जीवन जीना। ध्यान योग की चरमावस्था में पहुँचने के लिए इन चार शर्त्तों का पूरा होना जरूरी है। अब आगे इन्हीं चार की विस्तृत व्याख्या- अगले श्लोकों के साथ।
परमानंद की प्राप्ति
प्रशान्त मनसं, शान्तरजसं, ब्रह्मभूतम् एवं अकल्मषम् में चार स्थितियाँ ऐसी हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद हर ध्यानयोगी परमानन्द को प्राप्त हो सकता है। आखिर यह परमानन्द है क्या जिसकी प्रशस्ति गीताकार ने इतनी अधिक गायी है। आत्मा- परमात्मा के मिलन संयोग को ही उनने उत्तम आनन्द माना है- परमानन्द कहा है। विषयों से मिलने वाले आनन्द से मनुष्य कभी अघाता नहीं, कभी भी तृप्ति उसे मिलती नहीं, उसकी शक्ति सदैव नष्ट होती रहती है। किंतु योगजन्य इस आनन्द से उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है एवं वह आनन्द की परमावस्था को प्राप्त हो तृप्ति, तुष्टि, शान्ति पाता है। इस आनन्द की प्राप्ति तभी संभव है जब मन चंचल होकर इधर उधर न भटके- शान्त हो, किसी भी पापकर्म में यह योगी उलझता न हो, जिसका रजोगुण शान्त होकर सतोगुण की अभिवृद्धि की मात्रा आरंभ हो गयी हो तथा जिसने स्वयं को ब्रह्ममय बना लिया हो- वह ब्रह्म के स्वरूप को ही प्राप्त हो गया हो।
पूरा आत्म संयम योग बार- बार मन को भटकने से रोककर उसे परमात्मसत्ता में- आदर्शों में निरुद्ध होने की बात करता है। जब तक हम अपना लक्ष्य उस सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा को नहीं बनायेंगे- उसी से एकाकार होने की भावना में मन को नियोजित नहीं कर देते वासनाएँ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक बार उस सौन्दर्य का दर्शन हो जाये- उस आनन्द का रसास्वादन हो जाये तो फिर सारे विषय- भोग उसके समक्ष तुच्छ लगने लगेंगे।
श्रीकृष्ण गीता में पहले भी स्थितप्रज्ञ प्रकरण में कह चुके हैं—‘‘रसवर्जं रमः अपि अस्य परदृष्ट्वा निवर्तते’’ (अध्याय 2 श्लोक ५९ बी) अर्थात् [जिनके विषय निवृत्त हो चुके हैं उनकी] उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती (रसवर्जं) [परन्तु] परब्रह्म का (परं) साक्षात्कार होने पर (दृष्ट्वा) इस स्थितप्रज्ञ योगी की (अस्य) विषय भोग की आसक्ति (रसः) भी (अपि) निवृत्त हो जाती है (निवर्तते)।
अमृतरस की वह एक बूँद
श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिसने अमृत रस की एक बूँद का स्वाद चख लिया उसे रम्भा एवं तिलोत्तमा भी चिता की भस्म के समान प्रतीत होती है। आसक्ति नष्ट होने के लिए भगवान के साथ अनुराग पैदा करना होगा। एक कथा इस संबंध में समझाने हेतु ठीक रहेगी। यह सत्यकथा है एवं श्री रामानुजाचार्य से जुड़ी है। श्रीरंगम् में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता था। उसमें रामानुज भी अपने शिष्यों के साथ जाते थे। एक दुर्दान्त डाकू जिसका नाम था दुर्दम् वह भी दर्शनों को आता पर उसका उद्देश्य अलग था। वह एक सुन्दर सी महिला, जो वेश्या थी, के पीछे छाता लगाकर चलता। सबका ध्यान तो श्रीरंगम की छवि की ओर रहता पर उसका ध्यान उस सुन्दर युवती में लगा रहता। थी भी वह अत्यन्त सुन्दर। कोई भी आतंक के कारण उस दस्यु से कुछ कह नहीं पाता था। जब आचार्य रामानुज को यह सब पता चला तो उनने शिष्यों से कहा- उसे बुलाओ। आचार्य की शक्ति से वह भी भयभीत था कि कहीं शाप न दे दें। फिर भी वह आया। आचार्य बोले- हमें बड़ा अचरज है कि सभी भगवान में सौन्दर्य का दर्शन कर रहे हैं और तुम एक महिला में आसक्त हो। दस्यु बोला- यह सुन्दरतम स्त्री है जिसमें मेरी आसक्ति है- मैं उसे चाहता भी हूँ। आचार्य बोले- हम इससे भी सुन्दर कुछ दिखादें तो तुम इसे छोड़ दोगे क्या? इतना कहकर उसे श्रीरंगम् की छवि के दर्शन हेतु ले गए। मूर्त्ति में श्रीकृष्ण की अपूर्व सुन्दर झलक देखकर वह भावविह्वल हो गया। आचार्य से बोला- अब तो इन्हीं को प्राप्त करना है। आचार्य बोले साधना तप जो बताया जाएगा करोगे तो ही यह रूप टिकेगा व तुम्हें सतत दीखता रहेगा।
उसने स्वीकृति दी। सारा जीवनक्रम बदल दिया। उस स्त्री से आचार्य के निर्देशानुसार शादी कर ली। सारा जीवन उसने सद्गृहस्थ होकर जिया। लोकसेवी के रूप में जीवन जीने लगा। प्रतिदिन आचार्य स्नान करने सेवक- शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर जाते। कावेरी से लौटते तो दुर्दम के कंधे पर हाथ रखकर आते। सभी आश्चर्य करते कि एक शूद्र- डाकू को साथ लेकर आते हैं। आचार्य ने कहा- वह बदल गया है- तुम उसका दिल देखो- उसमें भगवान बसते हैं। लोगों ने परीक्षा ली- एकडाकू दल लूटने हेतु उसके घर भेजा। पत्नी ने देखा कि डाका डालने दस्युगण आए हैं। दुर्दम बोला- आचार्य के भक्त वैष्णवजन आए हैं। हम सोने का नाटक करते रहें। उसके इन वाक्यों को सुनकर हृदय बदला हुआ देख सभी मान गए कि परमेश्वर के दर्शन से व्यक्ति कितना बदल सकता है।
परमात्मा के दिव्य सौन्दर्य का दर्शन मनुष्य में कितना परिवर्तन ला सकता है, प्रस्तुत दृष्टान्त इसका परिचायक है। इस दर्शन से प्राप्त होने वाले आनन्द को ही दिव्यानन्द कहा गया है।
प्रशान्त मनसं
जब भगवान इस महत्त्वपूर्ण सत्ताइसवें श्लोक में कहते हैं- ‘‘प्रशान्तमनसं’’ तो उनका आशय है- विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिन्तन छोड़कर और चंचलता- विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और प्रसन्न हो गया है- इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के दिव्य सौन्दर्य में अचल स्थिति हो गयी है। ऐसा व्यक्ति ‘‘प्रशान्त मनसं’’ कहलाता है। वह कभी भी अशान्त होकर तनावग्रस्त नहीं होता। उस पर उद्वेगों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता।
शान्तरजसं ब्रह्मभूतम्
‘‘शान्तरजसं’’ से आशय है- आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा, सकामकर्म जिनकी रजोगुण से उत्पत्ति होती है (चौदहवें अध्याय का सातवाँ एवं बारहवाँ श्लोक) एवं जो रजोगुण को सतत बढ़ाते हैं, इन सबसे योगी का मुक्त हो जाना। चंचलता रूपी विकार भी रजोगुण का ही परिचायक है। ‘‘ब्रह्मभूतम्’’ से आशय है- योगी देह मात्र नहीं है- सच्चिदानन्द घन ब्रह्म है, इस भाव का सतत निरन्तर अभ्यास करना। ऐसा करने से साधक उस परमात्मा में स्थित हो जाता है। अभिन्न भाव से सतत ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। ‘‘ब्रह्मभूतम्’’ पद किसी सिद्धि का परिचायक नहीं है। यह एक स्थिति है जिसमें सतत रहने पर तत्त्वज्ञान द्वारा योगी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
अकल्मषम्
इसी श्लोक में ‘‘अकल्मषम्’’ शब्द आया है। मनुष्य को पतन के गर्त्त में डालने वाले जो तमोगुण हैं- प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मोह, दुराचार आदि ये सभी कल्मष कहलाते हैं। इन कल्मषों से मुक्ति अर्थात् पाप से सर्वथा रहित। पापकर्म से सदैव के लिए मुक्ति अकल्मषम् का शाद्बिक अर्थ होता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें चार शर्त्तों को पारकर उत्तम सुख की प्राप्ति का उपाय बताता है। ध्यानजनित सात्विक आनन्द ही उत्तम सुख है। इसी को अक्षय आनन्द के रूप में पाँचवें अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में बताया गया था। इसी पाँचवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक में ‘‘योऽअन्तःसुखोऽन्तरात्मा’’ के रूप में भी प्रतिपादित किया गया था।
गीता गहन ज्ञान की एक ऐसी पुस्तिका है जो हमें लौकिक से पारलौकिक आनन्द की ओर ले जाती है, जो हमें सतत सतोगुण की अभिवृद्धि का उपाय बताती है एवं क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलना सिखाती है। यदि हम अर्जुन के माध्यम से योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा दिये जा रहे इस मार्गदर्शन को समझ सकें तो हमारा सतत कल्याण ही होगा। हम गृहस्थ जीवन या सामान्य ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए भी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उपनिषदों के समस्त ज्ञान का निचोड़ गीता के प्रत्येक श्लोक में है। ध्यान योग द्वारा साधक कैसे अपनी अन्तर्जगत की यात्रा को पूरा करे- कहाँ कहाँ उसे क्या सावधानियाँ रखनी हैं, यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गीता में कूट कूट कर भरा है।
ब्रह्मानन्द की ओर एक कदम
उत्तम सुख का झरना अंदर से फूट पड़े, यह बताने के बाद श्रीकृष्ण ऐसे साधकों को, जो संभवतः अब तक समग्र मार्गदर्शन समझ न पा रहे हों एक प्रकार से आश्वस्त करते हैं एवं पुनः ध्यानयोग में प्रवृत्त हो उस ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला श्लोक यही कहता है।
युज्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्रुते॥ गी० ६/२८
अर्थात्- इस प्रकार (एवं) अपने मन को (आत्मानं) सदा के लिए (सदा) आत्मा के साथ युक्त करके (युज्जन), निष्पाप होकर (विगतकल्मषः) योगी पुरुष (योगी) सहज ही (सुखेन) ब्रह्मस्वरूप (ब्रह्मसंस्पर्श) अत्यन्त (अत्यन्तं) आनन्द (सुखं) प्राप्त करते हैं (अश्रुते)।
भावार्थ संक्षेप में इस प्रकार हुआ- ‘‘इस प्रकार अपने मन को सदा आत्मा के साथ युक्त करके (आत्मा को परमात्मा में लगाकर) वह पापरहित योगी आसानी से (सहज ही) परब्रह्म परमात्मा की प्राप्तिरूपी अनन्त आनंद की अनुभूति करता है।’’
ऐसा साधक या योगी भूमानन्द में प्रतिष्ठित होता है। निर्विकल्प भूमि के परमानन्द में प्रतिष्ठित होता है। यह आश्वासन श्रीकृष्ण का है किसी भी ऐसे साधक को जो हिचकिचाहट के कारण इस फलश्रुति को न समझ पाया हो। जिस किसी ने भी चार शर्तें (श्लोक २७) पूरी करली हों, वह सहज भाव से ही ब्रह्म के संस्पर्श से प्राप्त होने वाले अनन्त आनन्द को प्राप्त हो जाता है। यह आश्वासन की पुनरावृत्ति है- योगेश्वर की हर ध्यान योगी के लिए एक प्रेरणा है।
‘‘युज्जनेवं ’’ से अर्थ है जो भगवान से जुड़ गया हो। जीव का ब्रह्म से- आत्मा का परमात्मा से जब मिलन- संयुक्तीकरण हो गया तो ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति हो जाती है। यह सबसे बड़ा सुख है। यदि हम इन्द्रिय सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं तो इसका अर्थ यह कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गयी है। भगवान कहते हैं- इस वियोग को संयोग में बदलो, तभी सच्चा सुख- ब्रह्मानन्द मिलेगा। जब यह सुख मिलेगा तो अनन्त आनन्द की प्राप्ति होगी। ‘‘लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गयी लाल’’ की तरह ऐसा लगने लगेगा- मानों चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा समाया है। ऐसी अनुभूति अनंत आनन्द को प्रदान करती है।
स्वार्थ से परमार्थ की ओर
सांसारिक कामनाओं के रहते सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता। उनके रहते तो लौकिक प्रेम, वासनाएँ- कामनाएँ ही पैदा होंगी एवं हम उनकी आग में जलते जलते यह सुरदुर्लभ जीवन नष्ट कर देंगे। मनोकामना पूर्त्ति के लिए किये गये भजन आदि- आध्यात्मिक उपचारों से तो हम अपना भिखारीपन ही बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि ‘‘तुम यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा को भजते हो तो तुम असली पुजारी हो। भिखारी से तुम पुजारी बनो।’’ भगवान से भगवान के लिए मिलो- मनोकामना के लिए नहीं। बड़ी चीज- ऊँची चीज पाने का प्रयास करो तो छोटे छोटे लाभ तो अनायास ही तुम्हें मिल जायेंगे। इसके लिए वे मार्ग भी बताते हैं- ‘‘शरीर को जहाँ भौतिक सुविधाओं और साधनों से सुख मिलता है, वहीं आत्मा को परमार्थ में सुखानुभूति होती है। जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट न किया जाएगा, उसकी माँग पूरी न की जाएगी तब तक सब सुखसुविधाएँ होते हुए भी मनुष्य को एक अभाव, एक अतृप्ति व्यग्र करती रहेगी। शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भर ही वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख है- आत्मा को संतुष्ट करना- उसे प्रसन्न करना। आत्मा को सुख का अनुभव आनन्द की अनुभूति का एक मात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यावहारिक स्वरूप है सेवा। जो काम उच्च और उज्ज्वल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे परमार्थ हैं। इसीलिये सेवाभावी का जीवन ही सफल और सार्थक कहा जा सकता है।’’ (सेवा साधना और उसके सिद्धान्त पृष्ठ ८)
वस्तुतः यह क्रान्तिकारी चिन्तन है। जब तक युगधर्म में नियोजन नहीं होगा- सेवा साधना नहीं होगी, व्यक्ति उस वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो गीता में बताया गया है। यह क्रान्तिकारी चिन्तन पूज्य आचार्यश्री का है। उनके इस चिन्तन ने लाखों व्यक्तियों को प्रज्ञापरिजन बना नवसृजन का निमित्त बना दिया।
महानता की प्राप्ति ही सच्चा सुख
इस अठ्ठाइसवें श्लोक में एक महत्त्वपूर्ण बात आयी है—आत्मा को निरन्तर परमात्मा में लगाने वाला (युज्जनेवं सदाऽत्मानं) परब्रह्म परमात्मा की प्राप्तिरूपी आनन्द की अनुभूति करता है (ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्रुते)। यहाँ श्रुति का एक वाक्य जानना जरूरी है-
‘‘यो वैभूमा तत्सुखं नाल्पेसुखमस्ति, भूमैव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः’’ (छान्दोाग्योपनिषद् ७/२३/१) अर्थात् ‘‘जो भूमा है (महान् निरतिशय है) वही सच्चा सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने का प्रयास करना चाहिए।’’ आगे उपनिषद्कार कहता है- जो भूमा है वही अमृत है, जो अल्प है, वही मरणशील है।
महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद् में कहते हैं- जो ब्रह्म को प्राप्त है उसको वह अनन्त असीम, अचिंत्य आनन्द प्राप्त है जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। यही वह अक्षय सुख है जो हर साधक का- योगी का अभीष्ट है- लक्ष्य है। वस्तुतः जब योगी देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है तब उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप स्थिति हो जाती है। इतना होते ही उसे सर्वोच्च आनन्द, अक्षय आनन्द सहजता से मिल जाता है। परंतु इसके लिए ‘‘विगतकल्मषः- पापरहित होना जरूरी है। जो रजोगुण से सतोगुण की यात्रा कर रहा है एवं जो ज्ञान की नौका में बैठा है, वह पापों से मुक्त रहता है।’’
ब्रह्मसंस्पर्श की फलश्रुति
अब जिसने ध्यान योग की यह सीढ़ी पार कर ली- उसकी स्थिति क्या होती है, परमात्मा से संस्पर्श रूपी आनन्द को प्राप्त होने के बाद उसकी लौकिक स्थिति क्या होती है, इसे श्रीकृष्ण अगले उन्तीसवें श्लोक में समझाते हैं-
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ गी० ६/२९
अर्थात- ऐसी समाधि में अवस्थित पुरुष (योग युक्तात्मा) चहुँ ओर (सर्वत्र) समभाव से ब्रह्म का दर्शनकर (समदर्शनः) अविद्या से उत्पन्न शरीरादि की सीमारहित आत्मा को (आत्मानम्) सभी प्राणियों में अवस्थित (सर्वभूतस्थम्) और सभी प्राणियों को (सर्वभूतानि च) अभिन्न रूप से आत्मा में (आत्मनि) दर्शन करते हैं (ईक्षते)।
इसका भावार्थ हुआ- ‘‘योगस्थित योगी सर्वत्र समदृष्टि वाला होता है। वह आत्मा को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है। थोड़ा विस्तार से भावार्थ समझें- ‘‘सर्वव्यापी अनन्तचेतन में एकीभाव से स्थितिरूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सबमें सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है।’’ (गीताप्रेस गोरखपुर की व्याख्या)
कितनी सुन्दर काव्य की अभिव्यंजना है,यहाँ। श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि जिसने ध्यान में सर्वोच्च अनुभूति प्राप्त करली, वह व्यक्ति तमाम परिस्थितियों में समदृष्टि से युक्त हो जाता है (सर्वत्र समदर्शनः) एवं संसार को अपने ही एक अंग के रूप में देखता है। ध्यान की यह सर्वोच्च उपलब्धि है। उसे अपने भीतर का आत्मा ही सबका आत्मा दिखाई देती है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है।
परमानंद की प्राप्ति
प्रशान्त मनसं, शान्तरजसं, ब्रह्मभूतम् एवं अकल्मषम् में चार स्थितियाँ ऐसी हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद हर ध्यानयोगी परमानन्द को प्राप्त हो सकता है। आखिर यह परमानन्द है क्या जिसकी प्रशस्ति गीताकार ने इतनी अधिक गायी है। आत्मा- परमात्मा के मिलन संयोग को ही उनने उत्तम आनन्द माना है- परमानन्द कहा है। विषयों से मिलने वाले आनन्द से मनुष्य कभी अघाता नहीं, कभी भी तृप्ति उसे मिलती नहीं, उसकी शक्ति सदैव नष्ट होती रहती है। किंतु योगजन्य इस आनन्द से उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है एवं वह आनन्द की परमावस्था को प्राप्त हो तृप्ति, तुष्टि, शान्ति पाता है। इस आनन्द की प्राप्ति तभी संभव है जब मन चंचल होकर इधर उधर न भटके- शान्त हो, किसी भी पापकर्म में यह योगी उलझता न हो, जिसका रजोगुण शान्त होकर सतोगुण की अभिवृद्धि की मात्रा आरंभ हो गयी हो तथा जिसने स्वयं को ब्रह्ममय बना लिया हो- वह ब्रह्म के स्वरूप को ही प्राप्त हो गया हो।
पूरा आत्म संयम योग बार- बार मन को भटकने से रोककर उसे परमात्मसत्ता में- आदर्शों में निरुद्ध होने की बात करता है। जब तक हम अपना लक्ष्य उस सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा को नहीं बनायेंगे- उसी से एकाकार होने की भावना में मन को नियोजित नहीं कर देते वासनाएँ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक बार उस सौन्दर्य का दर्शन हो जाये- उस आनन्द का रसास्वादन हो जाये तो फिर सारे विषय- भोग उसके समक्ष तुच्छ लगने लगेंगे।
श्रीकृष्ण गीता में पहले भी स्थितप्रज्ञ प्रकरण में कह चुके हैं—‘‘रसवर्जं रमः अपि अस्य परदृष्ट्वा निवर्तते’’ (अध्याय 2 श्लोक ५९ बी) अर्थात् [जिनके विषय निवृत्त हो चुके हैं उनकी] उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती (रसवर्जं) [परन्तु] परब्रह्म का (परं) साक्षात्कार होने पर (दृष्ट्वा) इस स्थितप्रज्ञ योगी की (अस्य) विषय भोग की आसक्ति (रसः) भी (अपि) निवृत्त हो जाती है (निवर्तते)।
अमृतरस की वह एक बूँद
श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिसने अमृत रस की एक बूँद का स्वाद चख लिया उसे रम्भा एवं तिलोत्तमा भी चिता की भस्म के समान प्रतीत होती है। आसक्ति नष्ट होने के लिए भगवान के साथ अनुराग पैदा करना होगा। एक कथा इस संबंध में समझाने हेतु ठीक रहेगी। यह सत्यकथा है एवं श्री रामानुजाचार्य से जुड़ी है। श्रीरंगम् में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता था। उसमें रामानुज भी अपने शिष्यों के साथ जाते थे। एक दुर्दान्त डाकू जिसका नाम था दुर्दम् वह भी दर्शनों को आता पर उसका उद्देश्य अलग था। वह एक सुन्दर सी महिला, जो वेश्या थी, के पीछे छाता लगाकर चलता। सबका ध्यान तो श्रीरंगम की छवि की ओर रहता पर उसका ध्यान उस सुन्दर युवती में लगा रहता। थी भी वह अत्यन्त सुन्दर। कोई भी आतंक के कारण उस दस्यु से कुछ कह नहीं पाता था। जब आचार्य रामानुज को यह सब पता चला तो उनने शिष्यों से कहा- उसे बुलाओ। आचार्य की शक्ति से वह भी भयभीत था कि कहीं शाप न दे दें। फिर भी वह आया। आचार्य बोले- हमें बड़ा अचरज है कि सभी भगवान में सौन्दर्य का दर्शन कर रहे हैं और तुम एक महिला में आसक्त हो। दस्यु बोला- यह सुन्दरतम स्त्री है जिसमें मेरी आसक्ति है- मैं उसे चाहता भी हूँ। आचार्य बोले- हम इससे भी सुन्दर कुछ दिखादें तो तुम इसे छोड़ दोगे क्या? इतना कहकर उसे श्रीरंगम् की छवि के दर्शन हेतु ले गए। मूर्त्ति में श्रीकृष्ण की अपूर्व सुन्दर झलक देखकर वह भावविह्वल हो गया। आचार्य से बोला- अब तो इन्हीं को प्राप्त करना है। आचार्य बोले साधना तप जो बताया जाएगा करोगे तो ही यह रूप टिकेगा व तुम्हें सतत दीखता रहेगा।
उसने स्वीकृति दी। सारा जीवनक्रम बदल दिया। उस स्त्री से आचार्य के निर्देशानुसार शादी कर ली। सारा जीवन उसने सद्गृहस्थ होकर जिया। लोकसेवी के रूप में जीवन जीने लगा। प्रतिदिन आचार्य स्नान करने सेवक- शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर जाते। कावेरी से लौटते तो दुर्दम के कंधे पर हाथ रखकर आते। सभी आश्चर्य करते कि एक शूद्र- डाकू को साथ लेकर आते हैं। आचार्य ने कहा- वह बदल गया है- तुम उसका दिल देखो- उसमें भगवान बसते हैं। लोगों ने परीक्षा ली- एकडाकू दल लूटने हेतु उसके घर भेजा। पत्नी ने देखा कि डाका डालने दस्युगण आए हैं। दुर्दम बोला- आचार्य के भक्त वैष्णवजन आए हैं। हम सोने का नाटक करते रहें। उसके इन वाक्यों को सुनकर हृदय बदला हुआ देख सभी मान गए कि परमेश्वर के दर्शन से व्यक्ति कितना बदल सकता है।
परमात्मा के दिव्य सौन्दर्य का दर्शन मनुष्य में कितना परिवर्तन ला सकता है, प्रस्तुत दृष्टान्त इसका परिचायक है। इस दर्शन से प्राप्त होने वाले आनन्द को ही दिव्यानन्द कहा गया है।
प्रशान्त मनसं
जब भगवान इस महत्त्वपूर्ण सत्ताइसवें श्लोक में कहते हैं- ‘‘प्रशान्तमनसं’’ तो उनका आशय है- विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिन्तन छोड़कर और चंचलता- विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और प्रसन्न हो गया है- इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के दिव्य सौन्दर्य में अचल स्थिति हो गयी है। ऐसा व्यक्ति ‘‘प्रशान्त मनसं’’ कहलाता है। वह कभी भी अशान्त होकर तनावग्रस्त नहीं होता। उस पर उद्वेगों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता।
शान्तरजसं ब्रह्मभूतम्
‘‘शान्तरजसं’’ से आशय है- आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा, सकामकर्म जिनकी रजोगुण से उत्पत्ति होती है (चौदहवें अध्याय का सातवाँ एवं बारहवाँ श्लोक) एवं जो रजोगुण को सतत बढ़ाते हैं, इन सबसे योगी का मुक्त हो जाना। चंचलता रूपी विकार भी रजोगुण का ही परिचायक है। ‘‘ब्रह्मभूतम्’’ से आशय है- योगी देह मात्र नहीं है- सच्चिदानन्द घन ब्रह्म है, इस भाव का सतत निरन्तर अभ्यास करना। ऐसा करने से साधक उस परमात्मा में स्थित हो जाता है। अभिन्न भाव से सतत ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। ‘‘ब्रह्मभूतम्’’ पद किसी सिद्धि का परिचायक नहीं है। यह एक स्थिति है जिसमें सतत रहने पर तत्त्वज्ञान द्वारा योगी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
अकल्मषम्
इसी श्लोक में ‘‘अकल्मषम्’’ शब्द आया है। मनुष्य को पतन के गर्त्त में डालने वाले जो तमोगुण हैं- प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मोह, दुराचार आदि ये सभी कल्मष कहलाते हैं। इन कल्मषों से मुक्ति अर्थात् पाप से सर्वथा रहित। पापकर्म से सदैव के लिए मुक्ति अकल्मषम् का शाद्बिक अर्थ होता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें चार शर्त्तों को पारकर उत्तम सुख की प्राप्ति का उपाय बताता है। ध्यानजनित सात्विक आनन्द ही उत्तम सुख है। इसी को अक्षय आनन्द के रूप में पाँचवें अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में बताया गया था। इसी पाँचवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक में ‘‘योऽअन्तःसुखोऽन्तरात्मा’’ के रूप में भी प्रतिपादित किया गया था।
गीता गहन ज्ञान की एक ऐसी पुस्तिका है जो हमें लौकिक से पारलौकिक आनन्द की ओर ले जाती है, जो हमें सतत सतोगुण की अभिवृद्धि का उपाय बताती है एवं क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलना सिखाती है। यदि हम अर्जुन के माध्यम से योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा दिये जा रहे इस मार्गदर्शन को समझ सकें तो हमारा सतत कल्याण ही होगा। हम गृहस्थ जीवन या सामान्य ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए भी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उपनिषदों के समस्त ज्ञान का निचोड़ गीता के प्रत्येक श्लोक में है। ध्यान योग द्वारा साधक कैसे अपनी अन्तर्जगत की यात्रा को पूरा करे- कहाँ कहाँ उसे क्या सावधानियाँ रखनी हैं, यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन गीता में कूट कूट कर भरा है।
ब्रह्मानन्द की ओर एक कदम
उत्तम सुख का झरना अंदर से फूट पड़े, यह बताने के बाद श्रीकृष्ण ऐसे साधकों को, जो संभवतः अब तक समग्र मार्गदर्शन समझ न पा रहे हों एक प्रकार से आश्वस्त करते हैं एवं पुनः ध्यानयोग में प्रवृत्त हो उस ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला श्लोक यही कहता है।
युज्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्रुते॥ गी० ६/२८
अर्थात्- इस प्रकार (एवं) अपने मन को (आत्मानं) सदा के लिए (सदा) आत्मा के साथ युक्त करके (युज्जन), निष्पाप होकर (विगतकल्मषः) योगी पुरुष (योगी) सहज ही (सुखेन) ब्रह्मस्वरूप (ब्रह्मसंस्पर्श) अत्यन्त (अत्यन्तं) आनन्द (सुखं) प्राप्त करते हैं (अश्रुते)।
भावार्थ संक्षेप में इस प्रकार हुआ- ‘‘इस प्रकार अपने मन को सदा आत्मा के साथ युक्त करके (आत्मा को परमात्मा में लगाकर) वह पापरहित योगी आसानी से (सहज ही) परब्रह्म परमात्मा की प्राप्तिरूपी अनन्त आनंद की अनुभूति करता है।’’
ऐसा साधक या योगी भूमानन्द में प्रतिष्ठित होता है। निर्विकल्प भूमि के परमानन्द में प्रतिष्ठित होता है। यह आश्वासन श्रीकृष्ण का है किसी भी ऐसे साधक को जो हिचकिचाहट के कारण इस फलश्रुति को न समझ पाया हो। जिस किसी ने भी चार शर्तें (श्लोक २७) पूरी करली हों, वह सहज भाव से ही ब्रह्म के संस्पर्श से प्राप्त होने वाले अनन्त आनन्द को प्राप्त हो जाता है। यह आश्वासन की पुनरावृत्ति है- योगेश्वर की हर ध्यान योगी के लिए एक प्रेरणा है।
‘‘युज्जनेवं ’’ से अर्थ है जो भगवान से जुड़ गया हो। जीव का ब्रह्म से- आत्मा का परमात्मा से जब मिलन- संयुक्तीकरण हो गया तो ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति हो जाती है। यह सबसे बड़ा सुख है। यदि हम इन्द्रिय सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं तो इसका अर्थ यह कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गयी है। भगवान कहते हैं- इस वियोग को संयोग में बदलो, तभी सच्चा सुख- ब्रह्मानन्द मिलेगा। जब यह सुख मिलेगा तो अनन्त आनन्द की प्राप्ति होगी। ‘‘लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गयी लाल’’ की तरह ऐसा लगने लगेगा- मानों चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा समाया है। ऐसी अनुभूति अनंत आनन्द को प्रदान करती है।
स्वार्थ से परमार्थ की ओर
सांसारिक कामनाओं के रहते सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता। उनके रहते तो लौकिक प्रेम, वासनाएँ- कामनाएँ ही पैदा होंगी एवं हम उनकी आग में जलते जलते यह सुरदुर्लभ जीवन नष्ट कर देंगे। मनोकामना पूर्त्ति के लिए किये गये भजन आदि- आध्यात्मिक उपचारों से तो हम अपना भिखारीपन ही बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि ‘‘तुम यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा को भजते हो तो तुम असली पुजारी हो। भिखारी से तुम पुजारी बनो।’’ भगवान से भगवान के लिए मिलो- मनोकामना के लिए नहीं। बड़ी चीज- ऊँची चीज पाने का प्रयास करो तो छोटे छोटे लाभ तो अनायास ही तुम्हें मिल जायेंगे। इसके लिए वे मार्ग भी बताते हैं- ‘‘शरीर को जहाँ भौतिक सुविधाओं और साधनों से सुख मिलता है, वहीं आत्मा को परमार्थ में सुखानुभूति होती है। जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट न किया जाएगा, उसकी माँग पूरी न की जाएगी तब तक सब सुखसुविधाएँ होते हुए भी मनुष्य को एक अभाव, एक अतृप्ति व्यग्र करती रहेगी। शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भर ही वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख है- आत्मा को संतुष्ट करना- उसे प्रसन्न करना। आत्मा को सुख का अनुभव आनन्द की अनुभूति का एक मात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यावहारिक स्वरूप है सेवा। जो काम उच्च और उज्ज्वल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे परमार्थ हैं। इसीलिये सेवाभावी का जीवन ही सफल और सार्थक कहा जा सकता है।’’ (सेवा साधना और उसके सिद्धान्त पृष्ठ ८)
वस्तुतः यह क्रान्तिकारी चिन्तन है। जब तक युगधर्म में नियोजन नहीं होगा- सेवा साधना नहीं होगी, व्यक्ति उस वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो गीता में बताया गया है। यह क्रान्तिकारी चिन्तन पूज्य आचार्यश्री का है। उनके इस चिन्तन ने लाखों व्यक्तियों को प्रज्ञापरिजन बना नवसृजन का निमित्त बना दिया।
महानता की प्राप्ति ही सच्चा सुख
इस अठ्ठाइसवें श्लोक में एक महत्त्वपूर्ण बात आयी है—आत्मा को निरन्तर परमात्मा में लगाने वाला (युज्जनेवं सदाऽत्मानं) परब्रह्म परमात्मा की प्राप्तिरूपी आनन्द की अनुभूति करता है (ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्रुते)। यहाँ श्रुति का एक वाक्य जानना जरूरी है-
‘‘यो वैभूमा तत्सुखं नाल्पेसुखमस्ति, भूमैव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः’’ (छान्दोाग्योपनिषद् ७/२३/१) अर्थात् ‘‘जो भूमा है (महान् निरतिशय है) वही सच्चा सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने का प्रयास करना चाहिए।’’ आगे उपनिषद्कार कहता है- जो भूमा है वही अमृत है, जो अल्प है, वही मरणशील है।
महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद् में कहते हैं- जो ब्रह्म को प्राप्त है उसको वह अनन्त असीम, अचिंत्य आनन्द प्राप्त है जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। यही वह अक्षय सुख है जो हर साधक का- योगी का अभीष्ट है- लक्ष्य है। वस्तुतः जब योगी देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है तब उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप स्थिति हो जाती है। इतना होते ही उसे सर्वोच्च आनन्द, अक्षय आनन्द सहजता से मिल जाता है। परंतु इसके लिए ‘‘विगतकल्मषः- पापरहित होना जरूरी है। जो रजोगुण से सतोगुण की यात्रा कर रहा है एवं जो ज्ञान की नौका में बैठा है, वह पापों से मुक्त रहता है।’’
ब्रह्मसंस्पर्श की फलश्रुति
अब जिसने ध्यान योग की यह सीढ़ी पार कर ली- उसकी स्थिति क्या होती है, परमात्मा से संस्पर्श रूपी आनन्द को प्राप्त होने के बाद उसकी लौकिक स्थिति क्या होती है, इसे श्रीकृष्ण अगले उन्तीसवें श्लोक में समझाते हैं-
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ गी० ६/२९
अर्थात- ऐसी समाधि में अवस्थित पुरुष (योग युक्तात्मा) चहुँ ओर (सर्वत्र) समभाव से ब्रह्म का दर्शनकर (समदर्शनः) अविद्या से उत्पन्न शरीरादि की सीमारहित आत्मा को (आत्मानम्) सभी प्राणियों में अवस्थित (सर्वभूतस्थम्) और सभी प्राणियों को (सर्वभूतानि च) अभिन्न रूप से आत्मा में (आत्मनि) दर्शन करते हैं (ईक्षते)।
इसका भावार्थ हुआ- ‘‘योगस्थित योगी सर्वत्र समदृष्टि वाला होता है। वह आत्मा को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है। थोड़ा विस्तार से भावार्थ समझें- ‘‘सर्वव्यापी अनन्तचेतन में एकीभाव से स्थितिरूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सबमें सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है।’’ (गीताप्रेस गोरखपुर की व्याख्या)
कितनी सुन्दर काव्य की अभिव्यंजना है,यहाँ। श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि जिसने ध्यान में सर्वोच्च अनुभूति प्राप्त करली, वह व्यक्ति तमाम परिस्थितियों में समदृष्टि से युक्त हो जाता है (सर्वत्र समदर्शनः) एवं संसार को अपने ही एक अंग के रूप में देखता है। ध्यान की यह सर्वोच्च उपलब्धि है। उसे अपने भीतर का आत्मा ही सबका आत्मा दिखाई देती है। यह अद्वैत की पराकाष्ठा है।
Versions
-
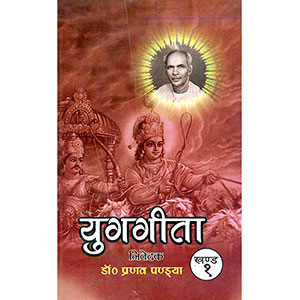
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
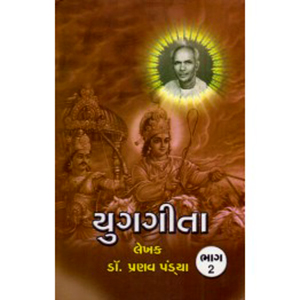
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
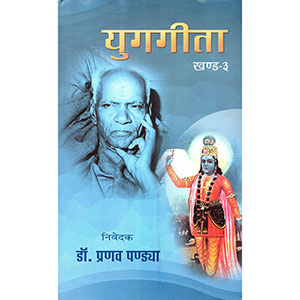
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
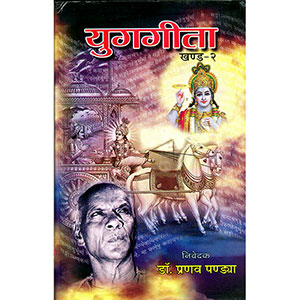
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
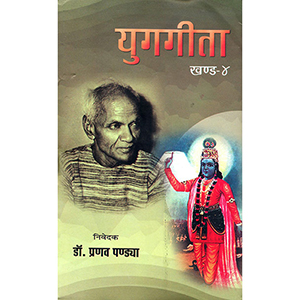
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
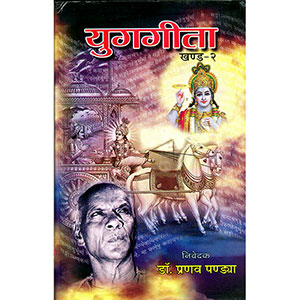
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
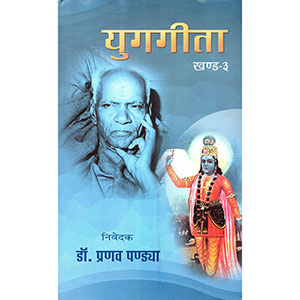
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
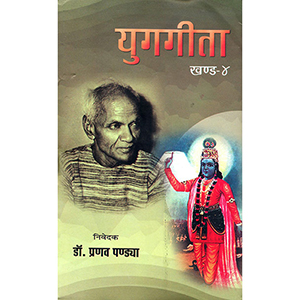
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
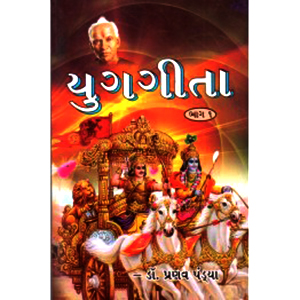
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- तृतीय खण्ड की प्रस्तावना
- प्रस्तुत चतुर्थ खण्ड की प्रस्तावना
- एकाकी यतचित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः
- ध्यान हेतु व्यावहारिक निर्देश देते एक कुशल शिक्षक
- सबसे बड़ा अनुदान परमानंद की पराकाष्ठा वाली दिव्य शांति
- युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
- कैसा होना चाहिए योगी का संयत चित्त
- योग की चरमावस्था की ओर ले जाते योगेश्वर
- परमात्मारूपी लाभ को प्राप्त व्यक्ति दुःख में विचलित नहीं होता
- बार-बार मन को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाए
- चित्तवृत्ति निरोध एवं परमानन्द प्राप्ति का राजमाग
- ध्यान की पराकाष्ठा पर होती है सर्वोच्च अनुभूति
- यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
- सुख या दुख में सर्वत्र समत्व के दर्शन करता है योगी
- कैसे आए यह चंचल मन काबू में?
- अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते
- कल्याणकारी कार्य करने वाले साधक की कभी दुर्गति नहीं होती
- भविष्य में हमारी क्या गति होगी, हम स्वयं निर्धारित करते हैं
- योग पथ पर चलने वाले का सदा कल्याण ही कल्याण है
- तस्मात् योगी भवार्जुन्
- वही ध्यानयोगी है श्रेष्ठ जो प्रभु को समर्पित है

