युगगीता - (भाग-२) 
पूर्ण तृप्त ज्ञानी की परिणति
Read Scan Version
‘ज्ञान में कर्मों का संन्यास’
जिस योग का अभीष्ट ध्येय हो, उस चौथे अध्याय की पराकाष्ठा पर
हम पहुँचते हैं जब भगवान् हमें बताते हैं कि इस संसार में
ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। अंतिम पाँच श्लोक वह राजमार्ग प्रशस्त करते हैं जो किसी भी साधक की जीवनयात्रा
बन सकता है। ज्ञान की परिपूर्णता पर पहुँचा हुआ साधक अंततः
क्या प्राप्त करता है, क्या उसकी परिणति होती है, यह हम इन तीन श्लोकों में पाते हैं।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ ४/३८
अर्थात्- ‘‘इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र निस्सन्देह कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त (शुद्ध अंतःकरण वाला) मनुष्य उस ज्ञान को अपने आप ही यथा समय अपनी आत्मा में पा लेता है।’’
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ४/३९
अर्थात्- ‘‘जो श्रद्धावान् है, तत्पर- साधन परायण है तथा जितेन्द्रिय (परिपूर्ण संयमशील) है, वह मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अविलम्ब ही तत्काल भगवत्प्राप्ति रूपी परमशान्ति को प्राप्त हो जाता है।’’
अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ ४/४०
अर्थात्- ‘‘श्रद्धाहीन अज्ञानी (विवेकरहित) तथा संशययुक्त मनुष्य परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। ऐसे संशयशील व्यक्ति के लिये न तो यह लोक है, न परलोक ही और उसे कहीं भी किसी भी काल में सुख की प्राप्ति नहीं होती।’’
ज्ञान की परिणति अंतः की शुद्धता
भगवान् बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वाधिक पवित्र यदि कुछ है तो वह ज्ञान ही है। यह ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। गुरु के उपदेश से जो ज्ञान मिलता है, उससे मनुष्य स्वतः शुद्ध होता चला जाता है। ‘‘कालेनात्मनि’’ शब्द का अर्थ है- अपने आप समय आने पर। हमें निरन्तर स्वयं को गुरु चेतना से ओतप्रोत रखना चाहिए; क्योंकि यही ज्ञान पवित्रतम है, सर्वश्रेष्ठ निधि है- पापनाशक है एवं हमें बड़े सौभाग्य से मिली है। गुरु पर परिपूर्ण श्रद्धा रख जो उनके बताए ज्ञान के पथ पर चलता रहता है, उसे आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है वह विनाश की राह पर कभी नहीं जाता। गुरु- शिष्यों का इतिहास हम देख लें तो यही पाते हैं कि वे निरन्तर अपने शिष्यों के आत्मकल्याण हेतु उन्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते रहे। उन्हें पवित्रतम ज्ञान का संदेश अपने आचरण से देते रहे। भगवान् यहाँ यही कह रहे हैं कि यह ज्ञान ज्यों- ज्यों कर्मयोग में सिद्ध पुरुष अपने अंदर प्रविष्ट करने लगता है उसे स्वयं यह अनुभूति होने लगती है (आत्मनि विन्दति)। ब्रह्मज्ञान एक अति दुर्लभ वस्तु है। ठाकुर श्रीरामकृष्ण देव ने एक स्थान पर कहा है- ‘‘नित्यवस्तु में पहुँचने का नाम ब्रह्मज्ञान है। यह बहुत कठिन है। एक- दम विषयबुद्धि न छूटने से वैसी अवस्था नहीं बन पाती। इसके लिये तपस्या चाहिए। शास्त्र के श्लोक कण्ठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। सिद्धि- सिद्धि कहने मात्र से नशा नहीं होगा। सिद्धि तो खानी चाहिए। उसकी अनुभूति कण- कण में होनी चाहिए।’’
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ‘‘ज्ञान को सत्शक्ति कहा गया है। मनुष्य की सच्ची सम्पत्ति कहा गया है। संसार में हर वस्तु काल पाकर नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है- तन जर्जर हो जाता है- साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्त्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता।’’ (( ‘‘आत्मोत्कर्ष का आधार- ज्ञान’’ वाङ्मय खण्ड ५८ पृष्ठ १०/२)। वस्तुतः मुक्ति का साधन है ज्ञान। इसे पा लिया तो इसी जीवन में मुक्ति मिल गई, ऐसा समझना चाहिए। एक बार ज्ञान का रसास्वादन करने पर मनुष्य इसी प्रकार तृप्त हो जाता है जिस प्रकार कोई प्यासा सुन्दर- स्वच्छ जलाशय को पाकर प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य का जीवन पाकर भी जिसने ज्ञान की कुछ बूँदें भी इकट्ठी न की हों, उसने तो मानो इस रत्न को मिट्टी के मोल खो दिया।
स्वयं को देह मत मानो, और गहरे जाओ
ज्ञान पवित्रतम है- आनन्द का कारण है एवं मुक्ति का आधार है। अज्ञान अथवा अविद्या को तो घोर अशान्ति का कारण माना गया है। जब संसार की साधारण बातों में अज्ञान हमें घोर दुःख देता है, तब जीवन- आत्मा और परमात्मा के विषय में संव्याप्त अज्ञान कितना भयंकर हो सकता है, इसकी तो मात्र कल्पना भर ही की जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान है अपने को देह मात्र मानकर चलना। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को विषयों में तृप्त करने में लगे रहकर अपनी आत्मा का नाश किया करते हैं।
आत्मज्ञान जब मनुष्य अपने अंदर पाने लगता है तो सबसे पहली उपलब्धि होती है- अंतःकरण की शुद्धि। यह कार्य स्वतः होने लगता है। पवित्रता का स्पर्श मात्र ही व्यक्ति को अंदर से शुद्ध बनाने लगता है और फिर वह उस आत्मज्ञान की अनुभूति अपने अंदर ही करने भी लगता है। योग द्वारा यह संसिद्धि उसे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। सकाम कर्मों की वासनाएँ भस्म होने लगती हैं। शुद्ध आत्मज्ञान के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है एवं फिर वही श्रीकृष्ण जो अभी चौंतीसवें श्लोक में ज्ञान को पाने का उपाय तत्त्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उनकी सेवा- दीक्षा लेने के माध्यम से बता रहे थे, (ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः) कहने लगते हैं कि वास्तविक ज्ञान तो हे अर्जुन! हमें अपने अंदर से ही मिलता है। अर्थात् यह ज्ञान उस साधक में, दिव्यकर्मी में संवर्द्धित होता रहता है और ज्यों- ज्यों वह निष्काम भाव में, समता में और भगवद्भक्ति में बढ़ता जाता है- त्यों त्यों ज्ञान की गहराई में भी प्रविष्ट होता चला जाता है? परंतु यह ज्ञान मिले कैसे? और उसकी अनुभूति हृदय की अंतरतम गहराईयों से कैसे हो? इसके लिये श्रीकृष्ण अगला सूत्र देते हैं।
वे कहते हैं कि यह ज्ञान श्रद्धावान् को ही प्राप्त होता है, बुद्धिमान को नहीं। जो ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि से बटोरता है वह तो इन्द्रियों व तर्कशक्तियों द्वारा परिश्रम करके बाहर से इकट्ठा किया जाता है। यह तो शिक्षा है- जानकारियाँ हैं। जो ज्ञान आत्मा में पाया जाता है- वह विद्या है। एवं यह विद्या अमरत्व का ज्ञान श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। यह कहा जाय कि जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह तुच्छ अहंकार को बाहर निकाल फेंकता है- मटियामेट कर देता है- व्यक्ति को श्रद्धाभाव से भर देता है, कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कोई अकारण नहीं कि यह चर्चा श्रीकृष्ण ज्ञान में कर्मों का न्यास- अर्पण नामक योग की अंतिम कुछ शिक्षाओं में साररूप में कर रहे हैं। इससे कम में आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति हम अपने भीतर नहीं कर पायेंगे।
श्रद्धावान् को मिलता है ज्ञान
उन्तालीसवें श्लोक द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञान प्राप्ति की कुछ अनिवार्य शर्तें सामने रखते हैं। वे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति उसी साधक को होती है जो श्रद्धावान् है- तत्पर है- साधन पारायण है तथा संयतेन्द्रिय है। परम तत्त्व की खोज की ओर प्रेरित करती है श्रद्धा। बौद्धिक ज्ञान को निजी अनुभव में परिणित करने तथा आत्मज्ञान द्वारा उसी की पुष्टि की प्रक्रिया श्रद्धा का जागरण करती है। विनोबा कहते हैं- ‘‘अनुभव तर्कातीत है। श्रद्धा अनुभव के आधार पर रहने वाली; पर उससे भी परे की वस्तु है। ’’ (विचार पोथी, २०)। आखिर श्रद्धा की परिभाषा क्या है? पं० रामचंद्र शुक्ल कहते हैं- ‘‘किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण तथा शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनन्द पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं।
श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ- साथ पूज्य बुद्धि का संचार भी है।’’ (चिंतामणि भाग- १) महात्मा गाँधी कहते हैं- श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्न- भिन्न हैं। श्रद्धा से अंतःज्ञान- आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिये अंतःशुद्धि तो होती ही है। बुद्धि से सृष्टि के ज्ञान- बाह्य के ज्ञान की वृद्धि होती है; परंतु उसका अंतःशुद्धि के साथ कार्य- कारण जैसा संबंध भी नहीं रहता। अत्यन्त बुद्धिमान लोग भी अत्यन्त चरित्र भ्रष्ट पाये जाते हैं; मगर श्रद्धा के साथ चरित्रशून्यता का होना असंभव है। ’’ (संपूर्ण गांधी वाङ्मय खण्ड ४१, पृष्ठ ८२)।
‘‘श्रद्धा’’ के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं- ‘‘अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति ही सर्वोपरि है। साधना से सिद्धि का मूलभूत आधार श्रद्धा है। मनुष्य का व्यक्तित्व जिसमें संस्कारों का (आदतों का) गहरा पुट रहता है, वस्तुतः श्रद्धा की परिपक्वता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।’’ आगे वे कहते हैं- ‘‘साधना का विशालकाय कलेवर इसलिये खड़ा किया गया है कि उन लौह श्रृंखलाओं में जकड़कर श्रद्धा- विश्वास रूपी महादैत्य को उपयोगी प्रयोजन उत्पन्न कर सकने के लिये प्रशिक्षित किया जा सके। श्रद्धा से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आत्मा का सबसे विश्वस्त और घनिष्ठ सचिव श्रद्धा ही है।’’ (पं० श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय- ‘‘उपासना ३ पृष्ठ ३.३२,३३)। कितनी सुन्दर व्याख्या श्रद्धा की हुई है और हमें बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन भी देती है कि श्रद्धावान् कैसे बनें?- कैसे श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करें।
सुत्त निपात (१/४/२) कहता है ‘‘श्रद्धा बीजं तपोबुद्धिः’’ अर्थात् श्रद्धा बीज है, तपश्चर्या है तथा ‘‘सद्धाय तरती ओधं’’ अर्थात् मनुष्य श्रद्धा से संसार प्रवाह को पार कर जाता है। (१/१०/२ सुत्तनिपात)। ऐतरेय ब्राह्मण (७/१०)कहता है- ‘‘श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान। श्रद्धा और सत्य का यह अत्यंत उत्तम जोड़ा है। श्रद्धा और सत्य के जोड़े से मनुष्य स्वर्ग को जीत लेता है।’’ ऋग्वेद कहता है- ‘‘श्रद्धा हृदयमयाकृत्या, श्रद्धया विन्दते वसु’’ (१०/१५१/१४) अर्थात् ‘‘सब लोग हृदय के दृढ़ संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।’’ गीताकार ने भी इसी श्रद्धा शब्द की व्याख्या १७वें अध्याय में ‘‘सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत’’ (१७/३) कह कर की है।
श्रद्धा ही नहीं, तत्परता व संयम भी
इस तरह श्रद्धा का महत्त्व समझ लेने पर जाना जा सकता है कि श्रद्धावान् को ही सच्चा आत्मज्ञान क्यों मिलता है। श्रद्धा के साथ श्रीकृष्ण दो बातें और बताते हैं- तत्पर होना तथा जितेन्द्रिय- संयमी होना। परमतत्व की खोज के लिये तत्परता- साधन परायणता जरूरी है। एकनिष्ठ भाव से साधनाशील होना अनिवार्य है। हो सकता है श्रद्धा एवं भक्तिभाव से ध्यान साधना के क्षेत्र में अधिकतम आंतरिक जागरूकता मिल भी जाय पर यदि इंद्रियाँ भलीभाँति नियंत्रित नहीं हैं तो न केवल एकाग्रता छिन्न- भिन्न हो जाती है- हम उस शान्ति को प्राप्त नहीं कर पाते जो आत्मज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि है। देखा जाये तो इन्द्रियों का स्वभाव ही बहिर्मुखी होना है। वे बार- बार विषयों की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं। इसीलिये जब तक हम इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं करते, तब तक लक्ष्य के प्रति श्रद्धा- असीम भक्ति भी हमें वांछित शान्ति प्रदान नहीं कर सकती।
ज्ञान को प्राप्त होने का साधन है श्रद्धा- गुरु के प्रति- शास्त्र वचनों के प्रति अटूट निष्ठा- आदर्शों से असीम प्यार एवं साधना में गति होने- इन्द्रिय संयम- अर्थ संयम- समय संयम एवं विचार संयम साध लेने पर सर्वोच्च स्तर की उपलब्धि हमें मिलती है- वह है शान्ति (परांशान्तिम्)। सारी विकलताओं से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, दुःखों से छुटकारा हमें मिल जाता है। संक्षोभ- विक्षोभ ही हमें विकल- रोगी बनाते हैं। यदि संत्रास मन से समाप्त हो जायँ तो हम सभी आधि- व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। आज सारा संसार इसी की तलाश में तो है। यह शांति कहाँ किसी को सहज ही सुलभ है। सारा जगत् अशांतिमय है- चैन की नींद कहाँ किसी को आती है। सारा जीवन परिग्रह में बीत गया- तृष्णा को पूरा करने में बीत गया- उसी कारण असंयमी बने तथा जीवनी शक्ति के स्रोतों को खोखला कर दिया। मन सदैव शंकाग्रस्त बना रहा- बुद्धि की प्रगति के क्षेत्र में तो चरम शिखर को छू लिया; पर श्रद्धा में गति हो नहीं पाई एवं यही कारण है कि सर्वत्र आज अशांति है- तनाव है- आतंक का साम्राज्य है।
कोई समाधान है तो वह गीताकार ही बताते हैं- श्रद्धावान् बनें- साधनाशील बनें तथा अपने ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें। इससे हम आदर्शों के- सद्वृत्तियों के समुच्चय परम पिता परमात्मा के ज्ञान से ओतप्रोत हो सकेंगे एवं यही ज्ञान मिलने पर अविलम्ब हमें भगवत्प्राप्ति होगी जो परम शांति की ओर हमें ले जाएगी।
अश्रद्धावान् का तो सुनिश्चित है सर्वनाश
किंतु शास्त्र ज्ञान रहित अज्ञानी, गुरु और वेदान्तरूपी तत्त्वदर्शन के वाक्यों में अश्रद्धा रखने वाला तथा सन्देहशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है, कभी ब्रह्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता- यह बात चालीसवें श्लोक में एक उद्घोषणा के रूप में श्रीकृष्ण करते हैं। आत्मज्ञानहीन जीवन श्रीकृष्ण की दृष्टि में मृत्युतुल्य और निरानन्दमय है। वह यह भी कहते हैं कि ऐसे अविश्वासी के लिये न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में ही सुख है। इस सीमा तक कह जाते हैं कि उसके लिये न तो यह संसार है, न अगला ही और उसे सुख की प्राप्ति की तो आशा ही नहीं करना चाहिए। कितनी आश्चर्य की बात है कि पशुओं को किसी प्रकार का संशय नहीं होता पर बुद्धि संपन्न मनुष्य सदैव, अधिकांश समय संशयी होता रहता है। संशय वहीं उठते हैं- जहाँ अभी स्पष्ट और सुनिश्चित ज्ञान का उदय न हुआ हो। इन संशयों से आखिर बाहर कौन निकाले? गुरुजन, शास्त्र, जाग्रत् महापुरुषों के प्रवचन, स्वाध्याय- ये सभी साधन हैं जो किसी भी साधक के हृदय की श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण ज्ञान हृदय द्वारा आत्मसात किया जाए और यह तभी संभव है जब साधक ध्यान में- शांत भाव से मनन करने में रुचि रखें। अध्ययन- मनन द्वारा एकत्र ज्ञान व्यवहार में लाने पर उसके प्रति निरन्तर श्रद्धा बढ़ती रहने पर सारे संशयों से निवृत्ति मिल जाती है।
जो बिना प्रश्र चिह्न लगाये गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता चलता है, यह मानता है कि उनके पास दिव्यदृष्टि है, तो उसका प्रगति का पथ- प्रशस्त होता चलता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल का मंच का अंतिम उद्बोधन देने १९८६ के वसंतपर्व पर आए थे और तब उनने कहा था कि ‘‘तुम्हारे पास दूरबीन हो तो मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जगत् में परिवर्तन हो चुका है। युग निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। तुम चाहो तो श्रेय ले लो। बस १५- २० वर्ष निरन्तर कार्य करते रहने भर की आवश्यकता है, फिर बदला जमाना तुम्हें दिखाई देने लगेगा।’’ यदि हमें गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है- हमारी श्रद्धा है- किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, तो हम उनकी शक्ति को अपने अंदर धारण कर वास्तव में अगले दिनों परिवर्तन का निमित्त कारण बनेंगे, हम भी यह देखेंगे, जमाना भी देखेगा; पर यदि हमें ही विश्वास न हो, हम ग्रहणशील न बन पाये हों तो हमारा विनाश- आत्मिक दृष्टि से अवगति- अधोगति सुनिश्चित है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं- ‘‘गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुख सिधि सुलभ न तेहि’’ अर्थात् जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास ही नहीं है, उसे प्रत्यक्ष तो क्या स्वप्र जगत् में भी सुख नहीं मिलता। वह अकारण दुःख पाता- निरन्तर कष्ट भोगता रहता है। कितने तो उदाहरण- नमूने हैं हमारे समक्ष जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास न रहा- वे गुरुद्रोही बने एवं अंततः कष्ट को प्राप्त हुए। कई ऐसे हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिये गुरु की बैसाखी लिए खड़े हैं, पर स्वयं अपने अंदर झाँकें तो पाते हैं कि उन्हें स्वयं गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। सिख धर्म पूरा गुरु के वचनों पर गहन विश्वास पर टिका है। यदि आज का युगधर्म निभना है तो वह युगपुरुष- हमारे गुरु के वचनों पर विश्वास- गहरी श्रद्धा टिकाने पर ही संभव हो सकेगा। अखण्ड ज्योति मई १९७० में पूज्यवर ने लिखा- ‘‘सद्भावनाओं का चक्रवर्ती सार्वभौम साम्राज्य जिस युगावतारी- निष्कलंक भगवान् द्वारा होने वाला है, वह और कोई नहीं, विशुद्ध रूप में अपना युग निर्माण आंदोलन ही है।’’ (पृष्ठ ६०) इसके बाद भी संशयात्मा हैं तो विनाश सुनिश्चित है।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ ४/३८
अर्थात्- ‘‘इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र निस्सन्देह कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त (शुद्ध अंतःकरण वाला) मनुष्य उस ज्ञान को अपने आप ही यथा समय अपनी आत्मा में पा लेता है।’’
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ४/३९
अर्थात्- ‘‘जो श्रद्धावान् है, तत्पर- साधन परायण है तथा जितेन्द्रिय (परिपूर्ण संयमशील) है, वह मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अविलम्ब ही तत्काल भगवत्प्राप्ति रूपी परमशान्ति को प्राप्त हो जाता है।’’
अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ ४/४०
अर्थात्- ‘‘श्रद्धाहीन अज्ञानी (विवेकरहित) तथा संशययुक्त मनुष्य परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। ऐसे संशयशील व्यक्ति के लिये न तो यह लोक है, न परलोक ही और उसे कहीं भी किसी भी काल में सुख की प्राप्ति नहीं होती।’’
ज्ञान की परिणति अंतः की शुद्धता
भगवान् बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वाधिक पवित्र यदि कुछ है तो वह ज्ञान ही है। यह ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। गुरु के उपदेश से जो ज्ञान मिलता है, उससे मनुष्य स्वतः शुद्ध होता चला जाता है। ‘‘कालेनात्मनि’’ शब्द का अर्थ है- अपने आप समय आने पर। हमें निरन्तर स्वयं को गुरु चेतना से ओतप्रोत रखना चाहिए; क्योंकि यही ज्ञान पवित्रतम है, सर्वश्रेष्ठ निधि है- पापनाशक है एवं हमें बड़े सौभाग्य से मिली है। गुरु पर परिपूर्ण श्रद्धा रख जो उनके बताए ज्ञान के पथ पर चलता रहता है, उसे आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है वह विनाश की राह पर कभी नहीं जाता। गुरु- शिष्यों का इतिहास हम देख लें तो यही पाते हैं कि वे निरन्तर अपने शिष्यों के आत्मकल्याण हेतु उन्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते रहे। उन्हें पवित्रतम ज्ञान का संदेश अपने आचरण से देते रहे। भगवान् यहाँ यही कह रहे हैं कि यह ज्ञान ज्यों- ज्यों कर्मयोग में सिद्ध पुरुष अपने अंदर प्रविष्ट करने लगता है उसे स्वयं यह अनुभूति होने लगती है (आत्मनि विन्दति)। ब्रह्मज्ञान एक अति दुर्लभ वस्तु है। ठाकुर श्रीरामकृष्ण देव ने एक स्थान पर कहा है- ‘‘नित्यवस्तु में पहुँचने का नाम ब्रह्मज्ञान है। यह बहुत कठिन है। एक- दम विषयबुद्धि न छूटने से वैसी अवस्था नहीं बन पाती। इसके लिये तपस्या चाहिए। शास्त्र के श्लोक कण्ठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। सिद्धि- सिद्धि कहने मात्र से नशा नहीं होगा। सिद्धि तो खानी चाहिए। उसकी अनुभूति कण- कण में होनी चाहिए।’’
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ‘‘ज्ञान को सत्शक्ति कहा गया है। मनुष्य की सच्ची सम्पत्ति कहा गया है। संसार में हर वस्तु काल पाकर नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है- तन जर्जर हो जाता है- साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्त्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता।’’ (( ‘‘आत्मोत्कर्ष का आधार- ज्ञान’’ वाङ्मय खण्ड ५८ पृष्ठ १०/२)। वस्तुतः मुक्ति का साधन है ज्ञान। इसे पा लिया तो इसी जीवन में मुक्ति मिल गई, ऐसा समझना चाहिए। एक बार ज्ञान का रसास्वादन करने पर मनुष्य इसी प्रकार तृप्त हो जाता है जिस प्रकार कोई प्यासा सुन्दर- स्वच्छ जलाशय को पाकर प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य का जीवन पाकर भी जिसने ज्ञान की कुछ बूँदें भी इकट्ठी न की हों, उसने तो मानो इस रत्न को मिट्टी के मोल खो दिया।
स्वयं को देह मत मानो, और गहरे जाओ
ज्ञान पवित्रतम है- आनन्द का कारण है एवं मुक्ति का आधार है। अज्ञान अथवा अविद्या को तो घोर अशान्ति का कारण माना गया है। जब संसार की साधारण बातों में अज्ञान हमें घोर दुःख देता है, तब जीवन- आत्मा और परमात्मा के विषय में संव्याप्त अज्ञान कितना भयंकर हो सकता है, इसकी तो मात्र कल्पना भर ही की जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान है अपने को देह मात्र मानकर चलना। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को विषयों में तृप्त करने में लगे रहकर अपनी आत्मा का नाश किया करते हैं।
आत्मज्ञान जब मनुष्य अपने अंदर पाने लगता है तो सबसे पहली उपलब्धि होती है- अंतःकरण की शुद्धि। यह कार्य स्वतः होने लगता है। पवित्रता का स्पर्श मात्र ही व्यक्ति को अंदर से शुद्ध बनाने लगता है और फिर वह उस आत्मज्ञान की अनुभूति अपने अंदर ही करने भी लगता है। योग द्वारा यह संसिद्धि उसे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। सकाम कर्मों की वासनाएँ भस्म होने लगती हैं। शुद्ध आत्मज्ञान के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है एवं फिर वही श्रीकृष्ण जो अभी चौंतीसवें श्लोक में ज्ञान को पाने का उपाय तत्त्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उनकी सेवा- दीक्षा लेने के माध्यम से बता रहे थे, (ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः) कहने लगते हैं कि वास्तविक ज्ञान तो हे अर्जुन! हमें अपने अंदर से ही मिलता है। अर्थात् यह ज्ञान उस साधक में, दिव्यकर्मी में संवर्द्धित होता रहता है और ज्यों- ज्यों वह निष्काम भाव में, समता में और भगवद्भक्ति में बढ़ता जाता है- त्यों त्यों ज्ञान की गहराई में भी प्रविष्ट होता चला जाता है? परंतु यह ज्ञान मिले कैसे? और उसकी अनुभूति हृदय की अंतरतम गहराईयों से कैसे हो? इसके लिये श्रीकृष्ण अगला सूत्र देते हैं।
वे कहते हैं कि यह ज्ञान श्रद्धावान् को ही प्राप्त होता है, बुद्धिमान को नहीं। जो ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि से बटोरता है वह तो इन्द्रियों व तर्कशक्तियों द्वारा परिश्रम करके बाहर से इकट्ठा किया जाता है। यह तो शिक्षा है- जानकारियाँ हैं। जो ज्ञान आत्मा में पाया जाता है- वह विद्या है। एवं यह विद्या अमरत्व का ज्ञान श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। यह कहा जाय कि जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह तुच्छ अहंकार को बाहर निकाल फेंकता है- मटियामेट कर देता है- व्यक्ति को श्रद्धाभाव से भर देता है, कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कोई अकारण नहीं कि यह चर्चा श्रीकृष्ण ज्ञान में कर्मों का न्यास- अर्पण नामक योग की अंतिम कुछ शिक्षाओं में साररूप में कर रहे हैं। इससे कम में आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति हम अपने भीतर नहीं कर पायेंगे।
श्रद्धावान् को मिलता है ज्ञान
उन्तालीसवें श्लोक द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञान प्राप्ति की कुछ अनिवार्य शर्तें सामने रखते हैं। वे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति उसी साधक को होती है जो श्रद्धावान् है- तत्पर है- साधन पारायण है तथा संयतेन्द्रिय है। परम तत्त्व की खोज की ओर प्रेरित करती है श्रद्धा। बौद्धिक ज्ञान को निजी अनुभव में परिणित करने तथा आत्मज्ञान द्वारा उसी की पुष्टि की प्रक्रिया श्रद्धा का जागरण करती है। विनोबा कहते हैं- ‘‘अनुभव तर्कातीत है। श्रद्धा अनुभव के आधार पर रहने वाली; पर उससे भी परे की वस्तु है। ’’ (विचार पोथी, २०)। आखिर श्रद्धा की परिभाषा क्या है? पं० रामचंद्र शुक्ल कहते हैं- ‘‘किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण तथा शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनन्द पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं।
श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ- साथ पूज्य बुद्धि का संचार भी है।’’ (चिंतामणि भाग- १) महात्मा गाँधी कहते हैं- श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्न- भिन्न हैं। श्रद्धा से अंतःज्ञान- आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिये अंतःशुद्धि तो होती ही है। बुद्धि से सृष्टि के ज्ञान- बाह्य के ज्ञान की वृद्धि होती है; परंतु उसका अंतःशुद्धि के साथ कार्य- कारण जैसा संबंध भी नहीं रहता। अत्यन्त बुद्धिमान लोग भी अत्यन्त चरित्र भ्रष्ट पाये जाते हैं; मगर श्रद्धा के साथ चरित्रशून्यता का होना असंभव है। ’’ (संपूर्ण गांधी वाङ्मय खण्ड ४१, पृष्ठ ८२)।
‘‘श्रद्धा’’ के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं- ‘‘अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति ही सर्वोपरि है। साधना से सिद्धि का मूलभूत आधार श्रद्धा है। मनुष्य का व्यक्तित्व जिसमें संस्कारों का (आदतों का) गहरा पुट रहता है, वस्तुतः श्रद्धा की परिपक्वता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।’’ आगे वे कहते हैं- ‘‘साधना का विशालकाय कलेवर इसलिये खड़ा किया गया है कि उन लौह श्रृंखलाओं में जकड़कर श्रद्धा- विश्वास रूपी महादैत्य को उपयोगी प्रयोजन उत्पन्न कर सकने के लिये प्रशिक्षित किया जा सके। श्रद्धा से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आत्मा का सबसे विश्वस्त और घनिष्ठ सचिव श्रद्धा ही है।’’ (पं० श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय- ‘‘उपासना ३ पृष्ठ ३.३२,३३)। कितनी सुन्दर व्याख्या श्रद्धा की हुई है और हमें बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन भी देती है कि श्रद्धावान् कैसे बनें?- कैसे श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करें।
सुत्त निपात (१/४/२) कहता है ‘‘श्रद्धा बीजं तपोबुद्धिः’’ अर्थात् श्रद्धा बीज है, तपश्चर्या है तथा ‘‘सद्धाय तरती ओधं’’ अर्थात् मनुष्य श्रद्धा से संसार प्रवाह को पार कर जाता है। (१/१०/२ सुत्तनिपात)। ऐतरेय ब्राह्मण (७/१०)कहता है- ‘‘श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान। श्रद्धा और सत्य का यह अत्यंत उत्तम जोड़ा है। श्रद्धा और सत्य के जोड़े से मनुष्य स्वर्ग को जीत लेता है।’’ ऋग्वेद कहता है- ‘‘श्रद्धा हृदयमयाकृत्या, श्रद्धया विन्दते वसु’’ (१०/१५१/१४) अर्थात् ‘‘सब लोग हृदय के दृढ़ संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।’’ गीताकार ने भी इसी श्रद्धा शब्द की व्याख्या १७वें अध्याय में ‘‘सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत’’ (१७/३) कह कर की है।
श्रद्धा ही नहीं, तत्परता व संयम भी
इस तरह श्रद्धा का महत्त्व समझ लेने पर जाना जा सकता है कि श्रद्धावान् को ही सच्चा आत्मज्ञान क्यों मिलता है। श्रद्धा के साथ श्रीकृष्ण दो बातें और बताते हैं- तत्पर होना तथा जितेन्द्रिय- संयमी होना। परमतत्व की खोज के लिये तत्परता- साधन परायणता जरूरी है। एकनिष्ठ भाव से साधनाशील होना अनिवार्य है। हो सकता है श्रद्धा एवं भक्तिभाव से ध्यान साधना के क्षेत्र में अधिकतम आंतरिक जागरूकता मिल भी जाय पर यदि इंद्रियाँ भलीभाँति नियंत्रित नहीं हैं तो न केवल एकाग्रता छिन्न- भिन्न हो जाती है- हम उस शान्ति को प्राप्त नहीं कर पाते जो आत्मज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि है। देखा जाये तो इन्द्रियों का स्वभाव ही बहिर्मुखी होना है। वे बार- बार विषयों की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं। इसीलिये जब तक हम इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं करते, तब तक लक्ष्य के प्रति श्रद्धा- असीम भक्ति भी हमें वांछित शान्ति प्रदान नहीं कर सकती।
ज्ञान को प्राप्त होने का साधन है श्रद्धा- गुरु के प्रति- शास्त्र वचनों के प्रति अटूट निष्ठा- आदर्शों से असीम प्यार एवं साधना में गति होने- इन्द्रिय संयम- अर्थ संयम- समय संयम एवं विचार संयम साध लेने पर सर्वोच्च स्तर की उपलब्धि हमें मिलती है- वह है शान्ति (परांशान्तिम्)। सारी विकलताओं से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, दुःखों से छुटकारा हमें मिल जाता है। संक्षोभ- विक्षोभ ही हमें विकल- रोगी बनाते हैं। यदि संत्रास मन से समाप्त हो जायँ तो हम सभी आधि- व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। आज सारा संसार इसी की तलाश में तो है। यह शांति कहाँ किसी को सहज ही सुलभ है। सारा जगत् अशांतिमय है- चैन की नींद कहाँ किसी को आती है। सारा जीवन परिग्रह में बीत गया- तृष्णा को पूरा करने में बीत गया- उसी कारण असंयमी बने तथा जीवनी शक्ति के स्रोतों को खोखला कर दिया। मन सदैव शंकाग्रस्त बना रहा- बुद्धि की प्रगति के क्षेत्र में तो चरम शिखर को छू लिया; पर श्रद्धा में गति हो नहीं पाई एवं यही कारण है कि सर्वत्र आज अशांति है- तनाव है- आतंक का साम्राज्य है।
कोई समाधान है तो वह गीताकार ही बताते हैं- श्रद्धावान् बनें- साधनाशील बनें तथा अपने ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें। इससे हम आदर्शों के- सद्वृत्तियों के समुच्चय परम पिता परमात्मा के ज्ञान से ओतप्रोत हो सकेंगे एवं यही ज्ञान मिलने पर अविलम्ब हमें भगवत्प्राप्ति होगी जो परम शांति की ओर हमें ले जाएगी।
अश्रद्धावान् का तो सुनिश्चित है सर्वनाश
किंतु शास्त्र ज्ञान रहित अज्ञानी, गुरु और वेदान्तरूपी तत्त्वदर्शन के वाक्यों में अश्रद्धा रखने वाला तथा सन्देहशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है, कभी ब्रह्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता- यह बात चालीसवें श्लोक में एक उद्घोषणा के रूप में श्रीकृष्ण करते हैं। आत्मज्ञानहीन जीवन श्रीकृष्ण की दृष्टि में मृत्युतुल्य और निरानन्दमय है। वह यह भी कहते हैं कि ऐसे अविश्वासी के लिये न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में ही सुख है। इस सीमा तक कह जाते हैं कि उसके लिये न तो यह संसार है, न अगला ही और उसे सुख की प्राप्ति की तो आशा ही नहीं करना चाहिए। कितनी आश्चर्य की बात है कि पशुओं को किसी प्रकार का संशय नहीं होता पर बुद्धि संपन्न मनुष्य सदैव, अधिकांश समय संशयी होता रहता है। संशय वहीं उठते हैं- जहाँ अभी स्पष्ट और सुनिश्चित ज्ञान का उदय न हुआ हो। इन संशयों से आखिर बाहर कौन निकाले? गुरुजन, शास्त्र, जाग्रत् महापुरुषों के प्रवचन, स्वाध्याय- ये सभी साधन हैं जो किसी भी साधक के हृदय की श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण ज्ञान हृदय द्वारा आत्मसात किया जाए और यह तभी संभव है जब साधक ध्यान में- शांत भाव से मनन करने में रुचि रखें। अध्ययन- मनन द्वारा एकत्र ज्ञान व्यवहार में लाने पर उसके प्रति निरन्तर श्रद्धा बढ़ती रहने पर सारे संशयों से निवृत्ति मिल जाती है।
जो बिना प्रश्र चिह्न लगाये गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता चलता है, यह मानता है कि उनके पास दिव्यदृष्टि है, तो उसका प्रगति का पथ- प्रशस्त होता चलता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल का मंच का अंतिम उद्बोधन देने १९८६ के वसंतपर्व पर आए थे और तब उनने कहा था कि ‘‘तुम्हारे पास दूरबीन हो तो मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ कि सूक्ष्म जगत् में परिवर्तन हो चुका है। युग निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। तुम चाहो तो श्रेय ले लो। बस १५- २० वर्ष निरन्तर कार्य करते रहने भर की आवश्यकता है, फिर बदला जमाना तुम्हें दिखाई देने लगेगा।’’ यदि हमें गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है- हमारी श्रद्धा है- किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, तो हम उनकी शक्ति को अपने अंदर धारण कर वास्तव में अगले दिनों परिवर्तन का निमित्त कारण बनेंगे, हम भी यह देखेंगे, जमाना भी देखेगा; पर यदि हमें ही विश्वास न हो, हम ग्रहणशील न बन पाये हों तो हमारा विनाश- आत्मिक दृष्टि से अवगति- अधोगति सुनिश्चित है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं- ‘‘गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुख सिधि सुलभ न तेहि’’ अर्थात् जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास ही नहीं है, उसे प्रत्यक्ष तो क्या स्वप्र जगत् में भी सुख नहीं मिलता। वह अकारण दुःख पाता- निरन्तर कष्ट भोगता रहता है। कितने तो उदाहरण- नमूने हैं हमारे समक्ष जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास न रहा- वे गुरुद्रोही बने एवं अंततः कष्ट को प्राप्त हुए। कई ऐसे हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिये गुरु की बैसाखी लिए खड़े हैं, पर स्वयं अपने अंदर झाँकें तो पाते हैं कि उन्हें स्वयं गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। सिख धर्म पूरा गुरु के वचनों पर गहन विश्वास पर टिका है। यदि आज का युगधर्म निभना है तो वह युगपुरुष- हमारे गुरु के वचनों पर विश्वास- गहरी श्रद्धा टिकाने पर ही संभव हो सकेगा। अखण्ड ज्योति मई १९७० में पूज्यवर ने लिखा- ‘‘सद्भावनाओं का चक्रवर्ती सार्वभौम साम्राज्य जिस युगावतारी- निष्कलंक भगवान् द्वारा होने वाला है, वह और कोई नहीं, विशुद्ध रूप में अपना युग निर्माण आंदोलन ही है।’’ (पृष्ठ ६०) इसके बाद भी संशयात्मा हैं तो विनाश सुनिश्चित है।
Versions
-
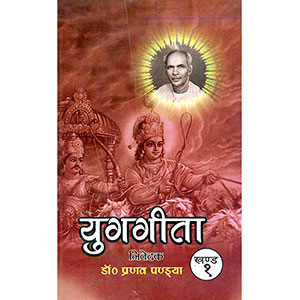
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
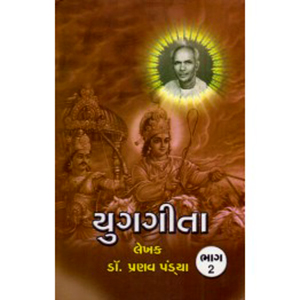
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
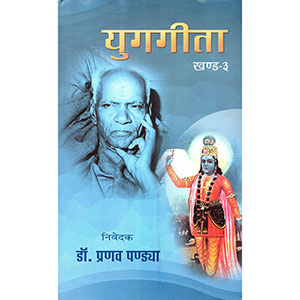
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
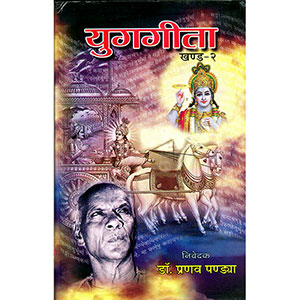
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
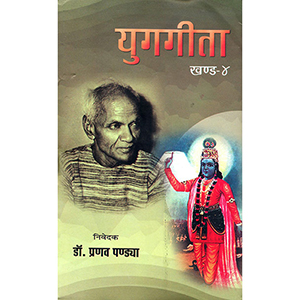
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
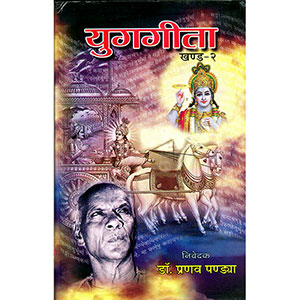
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
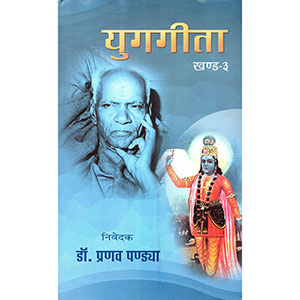
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
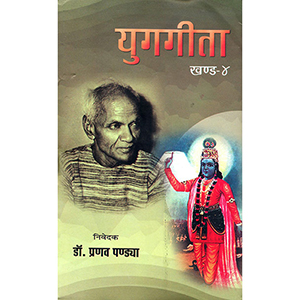
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
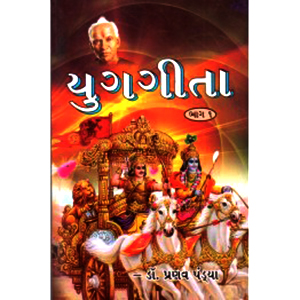
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- प्रस्तुत द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और किसलिए आए हो?
- धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
- जन्म कर्म च मे दिव्यम्
- वीतराग होने पर प्रभु के स्वरूप को प्राप्त होना
- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
- कर्म, अकर्म तथा विकर्म
- कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का मर्म
- गहना कर्मणोगति
- कैसे बनें दिव्यकर्मी और कैसे हों बंधनमुक्त
- कर्म में ब्रह्मदर्शन से ब्रह्म की ही प्राप्ति
- हर श्वास में संपादित दिव्य कर्म ही हैं यज्ञ
- यज्ञ बिना यह लोक नहीं तो परलोक कैसा?
- यज्ञों में श्रेष्ठतम-ज्ञानयज्ञ
- ज्ञान की नौका से भवसागर को पार करें
- पूर्ण तृप्त ज्ञानी की परिणति
- उठो भारत स्वयं को योग में प्रतिष्ठित करो

