युगगीता - (भाग-२) 
यज्ञ बिना यह लोक नहीं तो परलोक कैसा?
Read Scan Version
इकतीसवाँ श्लोक विशद व्याख्या हेतु पुनः प्रस्तुत हैः-
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम्॥ ४/३१
अर्थात्
‘‘हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिये तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है?’’
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च
एक छोटी सी कथा जो अक्सर परम वंदनीया माताजी अपनी ‘‘महायज्ञ’’ की व्याख्या के संदर्भ में उद्बोधन में सुनाया करती थीं, यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उपरोक्त श्लोक के भावार्थ को वह बड़ा स्पष्ट करती है। महाभारत में एक राजसूय यज्ञ की कथा आती है। साथ में एक नेवले का प्रसंग भी आता है। राजसूय यज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। युधिष्ठिर सहित पाण्डवों द्वारा संपन्न किया गया था। सभी के अहं बढ़चढ़कर बोल रहे थे कि हमारी वजह से यह आयोजन सफल हुआ। इतना दान हम लाए, इतना भोजन हमने कराया। हम लोग भी सत्ताइस अश्वमेध महायज्ञ कर चुके हैं, एक वाजपेय यज्ञ कर चुके हैं एवं अभी- अभी एक अश्वमेध तिरुपति में संपन्न किया है। कभी- कभी हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, बौरा जाते हैं कि यह सब हमने किया। गुरुसत्ता के प्रताप से ही जो कार्य हुआ हो, उसमें किसी को व्यक्तिगत अहंकार क्या पालना? पर अक्सर ऐसा हो जाता है, यही पाण्डवों के साथ हुआ। लेकिन भगवान् श्रीकृष्ण को लगा कि कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य रह गयी है, तभी तो यह अहंकार पल रहा है। एवं यह यज्ञ यज्ञीय भाव से नहीं हुआ- यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रीकृष्ण सभी को यज्ञ स्थल के पास ले गए। वहाँ सभी ने एक विचित्र स्थिति देखी। एक नेवला लोट रहा था। उसका आधा शरीर सोने का था, आधा सामान्य था। सभी उस विलक्षण प्राणी को देख रहे थे। भगवान से जानना चाह रहे थे कि यह क्या है, कैसे हुआ है? भगवान ने नेवले से उसी की भाषा में बात की। उसने मानवों को समझने में आ सकने वाली भाषा में कहा- ‘‘पहले भी मैंने एक महायज्ञ में भाग लिया था। उससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। यहाँ भी यही आशा लिये आया था कि बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाय। इसीलिये लोट लगा रहा हूँ, पर असफलता ही हाथ लगी है।’’
भगवान् कृष्ण ने उस विचित्र नेवले से पूछा कि बताओ पिछला यज्ञ कैसा था? उसने बताया कि ‘‘एक ब्राह्मण परिवार अनुष्ठान कर रहा था। भयंकर अकाल की स्थिति थी। ऐसे में उनने नौ दिन पश्चात् बचा हुआ भोजन लेने का विचार किया था। नवें दिन भावनात्मक पूर्णाहुति कर ज्योंही ब्राह्मण परिवार भोजन के लिए बैठा तो एक चांडाल सामने आ गया। चाण्डाल ने कहा हमें भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं। ब्राह्मण ने अपना भोजन उसे दे दिया। भोजन कर लेने के बाद उसने कहा पेट नहीं भरा, तो ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन सामने रख दिया। भोजन के पश्चात् पुनः चाण्डाल बोला- बड़ी तेज भूख लगी है। इस भोजन से भी शान्ति नहीं हुई। गृहस्थ ब्राह्मण के दोनों पुत्रों ने अपना भोजन जो कि अब अंतिम आस के रूप में सामने रखा था, चाण्डाल को दे दिया। चाण्डाल ने पूछा कि अब आप क्या खायेंगे भगवान्। ब्राह्मण ने कहा कि पानी पीकर ही परायण कर लेंगे। सोचेंगे भगवान् की यही इच्छा थी। अतिथि देवता भूखे चले जायें, यह कैसे हो सकता है? चाण्डाल ने भोजन समाप्त किया- ब्राह्मण को साधुवाद दिया एवं अच्छी तरह कुल्ला कर तृप्ति का भाव प्रकट किया।’’ नेवले ने आश्चर्य चकित सभी पाण्डवों सहित श्रीकृष्ण को बताया कि जिस स्थान पर उस चाण्डाल ने कुल्ला किया था, मैंने उसी में लोट लगायी थी तो मैं आधा सोने का हो गया। मैंने एक और दृश्य देखा कि ज्योंही ब्राह्मण देव सपरिवार चाण्डाल रूपी अतिथि को प्रणाम करने झुके तो उठने पर उनने वहाँ नारायण हरि को पाया। स्वयं भगवान् चाण्डाल का रूप धर ब्राह्मण परिवार की यज्ञीय वृत्ति को परखने आए थे।
प्रतिकूलताओं में भी यज्ञीय भाव जिसका जिन्दा हो जो देने की आकांक्षा रखता हो- भावनाएँ जिसकी पुष्ट हो वही सही अर्थों में देवता होते हैं- एवं ऐसे देवताओं के होते हुए दुर्भिक्ष होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भगवान् के कहते ही घनघोर घटाएँ बरसने लगीं एवं अकाल की स्थिति चली गयी। यह यज्ञ पुनः हो, इसकी प्रतीक्षा में युगों- युगों से कर रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि इस महायज्ञ में भी मैं अधूरी आकांक्षा व आधा कंचन का तन लिए जा रहा हूँ। यह कहकर नेवला चला गया। हतप्रभ पाण्डवों को भगवान् श्रीकृष्ण ने बताया कि देख लिया आपने अपना प्रताप। पहले यज्ञ के मर्म को समझिए तब आप महायज्ञ के सही अर्थों में यजमान बन सकेंगे। सभी के अहंकार गल गए व सभी ने यज्ञमय जीवन का मर्म जाना। इसीलिये शास्त्र कहता है- ‘‘महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।’’ यज्ञों में भी श्रेष्ठतम एवं महायज्ञ कहा जाने वाला वह कर्म है जो व्यक्ति को ब्राह्मणत्व के पद पर अधिष्ठित कर देता, उसके जीवन को ब्राह्मण प्रधान कर देता है। ब्राह्मणत्व अर्थात् आज के तथाकथित मनुवाद के नाम पर आलोचना करने वाले जाति- वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं- ज्ञान का संपादन करने वाला- देवताओं की रीति- नीति वाला जीवन जीने वाला। इसी चौथे अध्याय की प्रारंभिक टिप्पणियों में गुण कर्म विभागानुसार चार वर्णों के रचने की चर्चा (श्लोक क्रमांक- १३) भगवान् ने की है। यदि वह हम समझ लें तो हमें यज्ञ- महायज्ञ का सही मर्म भी समझ में आ सकेगा।
भगवान् इसके पूर्व तीसवें श्लोक तक विचित्र यज्ञों के माध्यम से यज्ञ का मर्म बताते बताते यहाँ इक्कीसवें श्लोक में उपरोक्त कथा का सार इस तरह कह देते हैं- ‘‘यज्ञ से बचे अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।’’ मानव जाति की समाज की सेवा स्वरूप किया गया श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। इसके परिणाम स्वरूप जो आत्मसंतोष- कीर्त्ति आदि प्राप्त होता है, वह यज्ञ- अवशिष्ट है। यही ‘‘प्रसाद’’ कहलाता है जो विभिन्न प्रकार के पूर्व में बताए गए बारह प्रकार के यज्ञों की परिणति स्वरूप प्राप्त होता है। शर्त एक ही है कि यह सभी यज्ञ निष्काम भाव से किये जाएँ। ‘‘यज्ञावशिष्ट’’ या ‘‘प्रसाद’’ का अर्थ है वह पदार्थ या तत्व जो मानसिक शांति दे, तृप्ति दे, तुष्टि दे। उस तरह यज्ञमय जीवन हमारी सभी वासनाओं का क्षय कर मन को अनिर्वचनीय शांति से भर देता है। वह शान्ति जिसकी खोज में आज सारा विश्व है, इसी यज्ञमय जीवन की रीति- नीति से मिलती है। वासनाओं का क्षय होते ही अंतिम परिणति के रूप में हमें समष्टिगत चैतन्य से एकाकार होने की सिद्धि भी (ब्रह्म सनातनम्) मिल जाती है।
यज्ञावशिष्ट अमृत है
भगवान् आगे कहते हैं कि हे कुरुओं में श्रेष्ठ! यज्ञ न करने वाले के लिये तो यह लोक भी न होने के समान है (नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य) तब परलोक की बात की क्या कही जाय? (कुतोऽन्यः)। इस एक पंक्ति में बड़े ही मर्म की बात बता दी गयी है। एक ही सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन किया गया है कि जो व्यक्ति समर्पण भाव से (यज्ञीय भाव से) कर्म करने को तैयार नहीं, उसे न तो इस संसार में वास्तविक लाभ है, (संतोषमय जीवन- प्रसन्नता अथवा तृप्ति मिल पाती है) न ही मरने के बाद वह शांति पाता है। वास्तविक प्रसन्नता- सफल जीवन जीने की अनुभूति की एक ही कुंजी है- यज्ञभाव में रहकर उद्यमपूर्वक सतत कर्म करते रहना (कुर्वन्नेवेह कर्माणि)। जिस समाज या राष्ट्र में युवाशक्ति- भोग में डूबे आम आदमी, विषयी- विलासी महत्वाकांक्षी- भोगप्रधान चिन्तन वाले होंगे, वह राष्ट्र या समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, फल- फूल नहीं सकता- यह श्रीकृष्ण की स्पष्ट घोषणा है। न ही ऐसे समाज से कुशल शासक- संगठन कर्त्ता, नेता निकल पायेंगे, न इस जगत में कभी शान्ति मिल पाएगी- चाहे उद्योग कितने ही बढ़ जाएँ, कितना ही आधुनिकीकरण यंत्रीकरण क्यों न हो जाए।
त्यागमय जीवन में प्रतिष्ठित हों, भोग में नहीं- आज की स्थिति की कितनी सुन्दर समीक्षा है इस श्लोक में। बार- बार एक ही बात भगवान् कह रहे हैं कि बाह्य सुखों में शान्ति नहीं- वहाँ तो भोगवादी अतृप्ति भरी तृष्णा है- बैचेनी है। आज सारा मानव समाज ‘‘स्ट्रेस’’ नामक महाव्याधि से पीड़ित है, जिसे देखिए वही देखने में स्वस्थ पर अंदर से रीता, खोखला एवं तनावग्रस्त। एक अविज्ञात भय हमारे सबके साथ जुड़ा है। चाहे भौतिक जगत में कितनी ही सफलताएँ मिल गयी हों। आत्मिक जगत सूखा मरुस्थल बन गया है। कारण अयज्ञीय भाव से किये गये कर्म ही हैं। यदि किसी समाज का, राष्ट्र का पुर्ननिर्माण होगा तो जीवन जीने के तरीके को बदल कर- जीवन को भोगमय से बदलकर त्याग की जीवन में प्रतिष्ठा करने से। एक जागरुक कर्मठ, कभी जगद्गुरु रहा भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी पराधीन है, भ्रष्टों में भी भ्रष्टतम है- इसकी कार्यकुशलता को मानो जंग लग गयी है। किस कारण यज्ञमय जीवन की उपेक्षा से। जीवन में यज्ञ अर्थात् परमार्थ के लिये किये गये सत्कर्मों की उपेक्षा से- एकाकी स्वार्थी जिंदगी जीने की रीति नीति से। श्रीमद्भगवदगीता ही आज की युवाशक्ति को भावी पीढ़ी को एक संकेत देती है कि यदि यह जीवन सुख के साथ शान्ति संतोषमय बनाना है तो जीवन में यज्ञ को स्थान दो, नहीं तो जन्म जन्मांतरों तक अतृप्ति एवं वासना के बंधन ढोने पड़ेंगे। ‘‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’’ (ईशावास्योपनिषद्) की उक्ति अनुसार जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा से ही मोक्ष या परम शांति मिलेगी। पश्चिमोन्मुखी मध्यम वर्ग एवं कम्प्यूटर युग में जी रही आज की पीढ़ी यदि सही अर्थों में भोग का आनन्द चाहती है, मानसिक शांति चाहती है तो उसे अपनी जीवन शैली आमूल चूल बदलनी होगी, यही संदेश गीता का हमें यहाँ मिलता है।
परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ विज्ञान को पुनःप्रतिष्ठा दी एवं यज्ञ को एक दर्शन के रूप में स्थापित किया, यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। अंधकार युग में जो विगत सहस्रों वर्षों से चला आ रहा था- बुद्ध एवं शंकराचार्य के आगमन के बावजूद यज्ञ की चिन्ह पूजा ही होती रही अथवा यज्ञ रूपी शब्द का अनर्थ किया जाता रहा। भारतीय संस्कृति के पिता माने जाने वाले यज्ञ को परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों के चिन्तन में दैनन्दिन जीवन में- उपासनात्मक उपचारों में स्थान दिलाया ताकि सतयुगी वातावरण बन सके। उनके जीवन के शुभारम्भ से अंत तक- उनके महाप्रयाण के बाद संपन्न हो रहे देवसंस्कृति दिग्विजयी पराक्रम तक उनके हर निर्धारण में हमें यज्ञ का तत्वदर्शन समाहित मिलता है। अग्रि को पूज्यवर ने शिक्षक बताते हुए अग्रिहोत्र को सही अर्थों में जन- जन को समझाया। अग्रिहोत्र मात्र ही यज्ञ नहीं है अपितु यज्ञ एक विराट अर्थों में समझी जाने वाली परिभाषा है, इस पर उनने गायत्री यज्ञ विधान, यज्ञ का ज्ञान- विज्ञान जैसी ग्रंथमालाएँ उस समय लिखीं, जब यज्ञ के नाम पर सकाम यज्ञों- पण्डावाद एवं लूटखसोट का माहौल था।
यज्ञ : एक दर्शन
वे अखण्ड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं- ‘‘जिस तरह अग्रि यज्ञ कुण्ड में प्रज्ज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानाग्रि अंतःकरण में तपाग्रि इन्द्रियों में तथा कर्माग्रि देह में प्रज्ज्वलित रहनी चाहिए, यही यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप है। अपनी संकीर्णता, अहंता, स्वार्थपरता को जो इस दिव्य अग्रि में होम देता है, वह बदले में इतना प्राप्त करता है, जिससे नर को नारायण की पदवी मिल सके।’’ (अप्रैल १९८१ पृष्ठ ४९)। आगे वे इसी क्रम में यज्ञ को विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन बताते हुए लिखते हैं- ‘‘यज्ञ में समाहित विचार एवं प्रेरणाएँ आस्था परिशोधन एवं आदर्शों की प्रतिष्ठापना का एक सशक्त माध्यम हैं। इसमें सन्निहित विचार प्रवाह में मनुष्य को श्रेष्ठ, उदार एवं उदात्त बनाने के सारे तत्व विद्यमान हैं। ऐसे किसी दर्शन की खोज करनी हो जो विवादों से रहित एवं बोधगम्य हो तो वह यज्ञदर्शन ही हो सकता है।’’ (अखण्ड ज्योति, सितम्बर १९८१, पृष्ठ ४७)। वे लिखते हैं कि ‘‘दान, देवपूजन और संगतिकरण का यज्ञीय दर्शन मनुष्य को उदार एवं उदात्त बनाने में हर दृष्टि से सक्षम है। इन तीनों सिद्धांतों में मानवी विकास के लिये असीम संभावनाएँ सन्निहित हैं। ’’ (उपरोक्त पृष्ठ ४९)
भगवान् श्रीकृष्ण ने इसी प्रकार यज्ञ की महत्ता बताते बताते अपने कथन की पूर्णता इन शब्दों में व्यक्त कर दी है कि जो यज्ञावशिष्ट अमृत का भोग करते हैं, वे ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं (यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्)। वे कह जाते हैं कि यज्ञ ही विश्व का विधान है, यज्ञ के बिना जीवन ही नहीं- पारलौकिक जीवन में भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। न लोक में प्रभुत्व मिल सकता है, न परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद वे कह जाते हैं कि ‘‘ब्रह्म के मुख में अर्थात् वेद की वाणी में इस प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं। उन सबको तू कर्म से अर्थात् मन इन्द्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा उत्पन्न जानना। किंतु यह भी जान ले कि परमात्मा कर्मादि से परे है- ऐसा जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो सकेगा।’’ (श्लोक ३२ का भावार्थ)
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ४/३२
इकत्तीसवें श्लोक की पराकाष्ठा के रूप में मुक्ति के राजमार्ग- इस बत्तीसवें श्लोक में देखने को मिलती है। ये सभी यज्ञ जो ऊपर बताए गए भगवान् विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण के अनुसार ब्रह्मा के मुख से निःसृत हुए हैं- उस अग्रि के मुख से जो सभी द्रव्यों को ग्रहण करती है। सर्वव्यापी ब्रह्म की सदायज्ञों में प्रतिष्ठित है। संसार के सभी प्रकार के कर्म परम पिता परमात्मा के उद्देश्य से अर्पित यज्ञ बन सकते हैं। यदि हम भोजन करें तो यह मानकर करें कि ब्रह्म को आहुति दे रहे हैं- जगज्जननी महाकाली को भोजन करा रहे हैं। यदि मार्ग पर चल रहे हों तो यह भावना करें कि जगन्माता की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक ये तीनों प्रकार के कर्म जब प्रभु की प्रसन्नता के लिये, ईश्वर में अर्पण बुद्धि से किये जायें तो सभी कर्मयज्ञ में परिणित हो जाते हैं। ऐसे यज्ञों का प्रतिफल पहले चित्त की शुद्धि तथा फिर आत्मोपलब्धि- जीवन्मुक्ति के रूप में मिलता है।
स्वामी विवेकानन्द ने इस विषय में काफी कुछ कहा है। गीता का कर्मयोग स्वामी जी के शब्दों में ‘‘वैज्ञानिक प्रणाली से किया गया एक कर्मानुष्ठान है। कर्मों का उद्देश्य है- मन के भीतर जो अन्तर्निहित शक्ति है- उसे प्रगट करना अर्थात् जीवात्मा का जागरण करना। जो कुछ करो- जो कुछ खाओ- जो कुछ हवन करो- जो कुछ तप करो- जो कुछ दो सभी मुझ भगवान् में अर्पण कर शान्तभाव से स्थित होकर रहो।’’
स्वामी जी जिस भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं- उसी का बोध श्रीकृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कराते हुए उसकी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सभी साधनों या यज्ञों को कर्मज मान- कर्म से जन्मा मान पर यह भी समझ कि ये सभी एक भगवान् की विशाल शक्ति से जन्मे हैं, उसी के द्वारा निर्दिष्ट हैं। उस भगवान् तत्व को तत्व से जान कर भलीभाँति समझकर स्वयं को समर्पित कर यज्ञीय भाव से यदि हर कर्म किया जाएगा तो लोभ- मोह के भवबंधनों से हमेशा के लिये जीवन्मुक्ति मिल जाएगी। (एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे)
गीताकार के काव्य का सौन्दर्य उसके शब्दों के गुंथन से बढ़कर उसके भावों की निरन्तर उच्चतर- उच्चतम सोपान पर चलते जाने के क्रम में दिखाई पड़ता है। यदि हम यह मर्म जान लें कि हमें कर्म क्यों करना है, किसके लिये करना है, यज्ञीय भाव से किये गये कर्म क्या होते हैं एवं जीवन को यदि बंधनों में बंधने से बचाकर मुक्ति का पथ प्रशस्त कैसे करना है तो हम जीवन दर्शन जान लेते हैं। इसी बात को भगवान् आगे बढ़ाते हुए तैतीसवें श्लोक में द्रव्यमय यज्ञ के रूप में सबसे नीची सीढ़ी एवं ज्ञानमय यज्ञ के रूप में सबसे ऊँची सीढ़ी बताते हैं।
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम्॥ ४/३१
अर्थात्
‘‘हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिये तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है?’’
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च
एक छोटी सी कथा जो अक्सर परम वंदनीया माताजी अपनी ‘‘महायज्ञ’’ की व्याख्या के संदर्भ में उद्बोधन में सुनाया करती थीं, यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उपरोक्त श्लोक के भावार्थ को वह बड़ा स्पष्ट करती है। महाभारत में एक राजसूय यज्ञ की कथा आती है। साथ में एक नेवले का प्रसंग भी आता है। राजसूय यज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। युधिष्ठिर सहित पाण्डवों द्वारा संपन्न किया गया था। सभी के अहं बढ़चढ़कर बोल रहे थे कि हमारी वजह से यह आयोजन सफल हुआ। इतना दान हम लाए, इतना भोजन हमने कराया। हम लोग भी सत्ताइस अश्वमेध महायज्ञ कर चुके हैं, एक वाजपेय यज्ञ कर चुके हैं एवं अभी- अभी एक अश्वमेध तिरुपति में संपन्न किया है। कभी- कभी हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, बौरा जाते हैं कि यह सब हमने किया। गुरुसत्ता के प्रताप से ही जो कार्य हुआ हो, उसमें किसी को व्यक्तिगत अहंकार क्या पालना? पर अक्सर ऐसा हो जाता है, यही पाण्डवों के साथ हुआ। लेकिन भगवान् श्रीकृष्ण को लगा कि कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य रह गयी है, तभी तो यह अहंकार पल रहा है। एवं यह यज्ञ यज्ञीय भाव से नहीं हुआ- यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रीकृष्ण सभी को यज्ञ स्थल के पास ले गए। वहाँ सभी ने एक विचित्र स्थिति देखी। एक नेवला लोट रहा था। उसका आधा शरीर सोने का था, आधा सामान्य था। सभी उस विलक्षण प्राणी को देख रहे थे। भगवान से जानना चाह रहे थे कि यह क्या है, कैसे हुआ है? भगवान ने नेवले से उसी की भाषा में बात की। उसने मानवों को समझने में आ सकने वाली भाषा में कहा- ‘‘पहले भी मैंने एक महायज्ञ में भाग लिया था। उससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। यहाँ भी यही आशा लिये आया था कि बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाय। इसीलिये लोट लगा रहा हूँ, पर असफलता ही हाथ लगी है।’’
भगवान् कृष्ण ने उस विचित्र नेवले से पूछा कि बताओ पिछला यज्ञ कैसा था? उसने बताया कि ‘‘एक ब्राह्मण परिवार अनुष्ठान कर रहा था। भयंकर अकाल की स्थिति थी। ऐसे में उनने नौ दिन पश्चात् बचा हुआ भोजन लेने का विचार किया था। नवें दिन भावनात्मक पूर्णाहुति कर ज्योंही ब्राह्मण परिवार भोजन के लिए बैठा तो एक चांडाल सामने आ गया। चाण्डाल ने कहा हमें भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं। ब्राह्मण ने अपना भोजन उसे दे दिया। भोजन कर लेने के बाद उसने कहा पेट नहीं भरा, तो ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन सामने रख दिया। भोजन के पश्चात् पुनः चाण्डाल बोला- बड़ी तेज भूख लगी है। इस भोजन से भी शान्ति नहीं हुई। गृहस्थ ब्राह्मण के दोनों पुत्रों ने अपना भोजन जो कि अब अंतिम आस के रूप में सामने रखा था, चाण्डाल को दे दिया। चाण्डाल ने पूछा कि अब आप क्या खायेंगे भगवान्। ब्राह्मण ने कहा कि पानी पीकर ही परायण कर लेंगे। सोचेंगे भगवान् की यही इच्छा थी। अतिथि देवता भूखे चले जायें, यह कैसे हो सकता है? चाण्डाल ने भोजन समाप्त किया- ब्राह्मण को साधुवाद दिया एवं अच्छी तरह कुल्ला कर तृप्ति का भाव प्रकट किया।’’ नेवले ने आश्चर्य चकित सभी पाण्डवों सहित श्रीकृष्ण को बताया कि जिस स्थान पर उस चाण्डाल ने कुल्ला किया था, मैंने उसी में लोट लगायी थी तो मैं आधा सोने का हो गया। मैंने एक और दृश्य देखा कि ज्योंही ब्राह्मण देव सपरिवार चाण्डाल रूपी अतिथि को प्रणाम करने झुके तो उठने पर उनने वहाँ नारायण हरि को पाया। स्वयं भगवान् चाण्डाल का रूप धर ब्राह्मण परिवार की यज्ञीय वृत्ति को परखने आए थे।
प्रतिकूलताओं में भी यज्ञीय भाव जिसका जिन्दा हो जो देने की आकांक्षा रखता हो- भावनाएँ जिसकी पुष्ट हो वही सही अर्थों में देवता होते हैं- एवं ऐसे देवताओं के होते हुए दुर्भिक्ष होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भगवान् के कहते ही घनघोर घटाएँ बरसने लगीं एवं अकाल की स्थिति चली गयी। यह यज्ञ पुनः हो, इसकी प्रतीक्षा में युगों- युगों से कर रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि इस महायज्ञ में भी मैं अधूरी आकांक्षा व आधा कंचन का तन लिए जा रहा हूँ। यह कहकर नेवला चला गया। हतप्रभ पाण्डवों को भगवान् श्रीकृष्ण ने बताया कि देख लिया आपने अपना प्रताप। पहले यज्ञ के मर्म को समझिए तब आप महायज्ञ के सही अर्थों में यजमान बन सकेंगे। सभी के अहंकार गल गए व सभी ने यज्ञमय जीवन का मर्म जाना। इसीलिये शास्त्र कहता है- ‘‘महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।’’ यज्ञों में भी श्रेष्ठतम एवं महायज्ञ कहा जाने वाला वह कर्म है जो व्यक्ति को ब्राह्मणत्व के पद पर अधिष्ठित कर देता, उसके जीवन को ब्राह्मण प्रधान कर देता है। ब्राह्मणत्व अर्थात् आज के तथाकथित मनुवाद के नाम पर आलोचना करने वाले जाति- वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं- ज्ञान का संपादन करने वाला- देवताओं की रीति- नीति वाला जीवन जीने वाला। इसी चौथे अध्याय की प्रारंभिक टिप्पणियों में गुण कर्म विभागानुसार चार वर्णों के रचने की चर्चा (श्लोक क्रमांक- १३) भगवान् ने की है। यदि वह हम समझ लें तो हमें यज्ञ- महायज्ञ का सही मर्म भी समझ में आ सकेगा।
भगवान् इसके पूर्व तीसवें श्लोक तक विचित्र यज्ञों के माध्यम से यज्ञ का मर्म बताते बताते यहाँ इक्कीसवें श्लोक में उपरोक्त कथा का सार इस तरह कह देते हैं- ‘‘यज्ञ से बचे अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।’’ मानव जाति की समाज की सेवा स्वरूप किया गया श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। इसके परिणाम स्वरूप जो आत्मसंतोष- कीर्त्ति आदि प्राप्त होता है, वह यज्ञ- अवशिष्ट है। यही ‘‘प्रसाद’’ कहलाता है जो विभिन्न प्रकार के पूर्व में बताए गए बारह प्रकार के यज्ञों की परिणति स्वरूप प्राप्त होता है। शर्त एक ही है कि यह सभी यज्ञ निष्काम भाव से किये जाएँ। ‘‘यज्ञावशिष्ट’’ या ‘‘प्रसाद’’ का अर्थ है वह पदार्थ या तत्व जो मानसिक शांति दे, तृप्ति दे, तुष्टि दे। उस तरह यज्ञमय जीवन हमारी सभी वासनाओं का क्षय कर मन को अनिर्वचनीय शांति से भर देता है। वह शान्ति जिसकी खोज में आज सारा विश्व है, इसी यज्ञमय जीवन की रीति- नीति से मिलती है। वासनाओं का क्षय होते ही अंतिम परिणति के रूप में हमें समष्टिगत चैतन्य से एकाकार होने की सिद्धि भी (ब्रह्म सनातनम्) मिल जाती है।
यज्ञावशिष्ट अमृत है
भगवान् आगे कहते हैं कि हे कुरुओं में श्रेष्ठ! यज्ञ न करने वाले के लिये तो यह लोक भी न होने के समान है (नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य) तब परलोक की बात की क्या कही जाय? (कुतोऽन्यः)। इस एक पंक्ति में बड़े ही मर्म की बात बता दी गयी है। एक ही सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन किया गया है कि जो व्यक्ति समर्पण भाव से (यज्ञीय भाव से) कर्म करने को तैयार नहीं, उसे न तो इस संसार में वास्तविक लाभ है, (संतोषमय जीवन- प्रसन्नता अथवा तृप्ति मिल पाती है) न ही मरने के बाद वह शांति पाता है। वास्तविक प्रसन्नता- सफल जीवन जीने की अनुभूति की एक ही कुंजी है- यज्ञभाव में रहकर उद्यमपूर्वक सतत कर्म करते रहना (कुर्वन्नेवेह कर्माणि)। जिस समाज या राष्ट्र में युवाशक्ति- भोग में डूबे आम आदमी, विषयी- विलासी महत्वाकांक्षी- भोगप्रधान चिन्तन वाले होंगे, वह राष्ट्र या समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, फल- फूल नहीं सकता- यह श्रीकृष्ण की स्पष्ट घोषणा है। न ही ऐसे समाज से कुशल शासक- संगठन कर्त्ता, नेता निकल पायेंगे, न इस जगत में कभी शान्ति मिल पाएगी- चाहे उद्योग कितने ही बढ़ जाएँ, कितना ही आधुनिकीकरण यंत्रीकरण क्यों न हो जाए।
त्यागमय जीवन में प्रतिष्ठित हों, भोग में नहीं- आज की स्थिति की कितनी सुन्दर समीक्षा है इस श्लोक में। बार- बार एक ही बात भगवान् कह रहे हैं कि बाह्य सुखों में शान्ति नहीं- वहाँ तो भोगवादी अतृप्ति भरी तृष्णा है- बैचेनी है। आज सारा मानव समाज ‘‘स्ट्रेस’’ नामक महाव्याधि से पीड़ित है, जिसे देखिए वही देखने में स्वस्थ पर अंदर से रीता, खोखला एवं तनावग्रस्त। एक अविज्ञात भय हमारे सबके साथ जुड़ा है। चाहे भौतिक जगत में कितनी ही सफलताएँ मिल गयी हों। आत्मिक जगत सूखा मरुस्थल बन गया है। कारण अयज्ञीय भाव से किये गये कर्म ही हैं। यदि किसी समाज का, राष्ट्र का पुर्ननिर्माण होगा तो जीवन जीने के तरीके को बदल कर- जीवन को भोगमय से बदलकर त्याग की जीवन में प्रतिष्ठा करने से। एक जागरुक कर्मठ, कभी जगद्गुरु रहा भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी पराधीन है, भ्रष्टों में भी भ्रष्टतम है- इसकी कार्यकुशलता को मानो जंग लग गयी है। किस कारण यज्ञमय जीवन की उपेक्षा से। जीवन में यज्ञ अर्थात् परमार्थ के लिये किये गये सत्कर्मों की उपेक्षा से- एकाकी स्वार्थी जिंदगी जीने की रीति नीति से। श्रीमद्भगवदगीता ही आज की युवाशक्ति को भावी पीढ़ी को एक संकेत देती है कि यदि यह जीवन सुख के साथ शान्ति संतोषमय बनाना है तो जीवन में यज्ञ को स्थान दो, नहीं तो जन्म जन्मांतरों तक अतृप्ति एवं वासना के बंधन ढोने पड़ेंगे। ‘‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’’ (ईशावास्योपनिषद्) की उक्ति अनुसार जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा से ही मोक्ष या परम शांति मिलेगी। पश्चिमोन्मुखी मध्यम वर्ग एवं कम्प्यूटर युग में जी रही आज की पीढ़ी यदि सही अर्थों में भोग का आनन्द चाहती है, मानसिक शांति चाहती है तो उसे अपनी जीवन शैली आमूल चूल बदलनी होगी, यही संदेश गीता का हमें यहाँ मिलता है।
परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ विज्ञान को पुनःप्रतिष्ठा दी एवं यज्ञ को एक दर्शन के रूप में स्थापित किया, यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। अंधकार युग में जो विगत सहस्रों वर्षों से चला आ रहा था- बुद्ध एवं शंकराचार्य के आगमन के बावजूद यज्ञ की चिन्ह पूजा ही होती रही अथवा यज्ञ रूपी शब्द का अनर्थ किया जाता रहा। भारतीय संस्कृति के पिता माने जाने वाले यज्ञ को परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों के चिन्तन में दैनन्दिन जीवन में- उपासनात्मक उपचारों में स्थान दिलाया ताकि सतयुगी वातावरण बन सके। उनके जीवन के शुभारम्भ से अंत तक- उनके महाप्रयाण के बाद संपन्न हो रहे देवसंस्कृति दिग्विजयी पराक्रम तक उनके हर निर्धारण में हमें यज्ञ का तत्वदर्शन समाहित मिलता है। अग्रि को पूज्यवर ने शिक्षक बताते हुए अग्रिहोत्र को सही अर्थों में जन- जन को समझाया। अग्रिहोत्र मात्र ही यज्ञ नहीं है अपितु यज्ञ एक विराट अर्थों में समझी जाने वाली परिभाषा है, इस पर उनने गायत्री यज्ञ विधान, यज्ञ का ज्ञान- विज्ञान जैसी ग्रंथमालाएँ उस समय लिखीं, जब यज्ञ के नाम पर सकाम यज्ञों- पण्डावाद एवं लूटखसोट का माहौल था।
यज्ञ : एक दर्शन
वे अखण्ड ज्योति पत्रिका में लिखते हैं- ‘‘जिस तरह अग्रि यज्ञ कुण्ड में प्रज्ज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानाग्रि अंतःकरण में तपाग्रि इन्द्रियों में तथा कर्माग्रि देह में प्रज्ज्वलित रहनी चाहिए, यही यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप है। अपनी संकीर्णता, अहंता, स्वार्थपरता को जो इस दिव्य अग्रि में होम देता है, वह बदले में इतना प्राप्त करता है, जिससे नर को नारायण की पदवी मिल सके।’’ (अप्रैल १९८१ पृष्ठ ४९)। आगे वे इसी क्रम में यज्ञ को विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन बताते हुए लिखते हैं- ‘‘यज्ञ में समाहित विचार एवं प्रेरणाएँ आस्था परिशोधन एवं आदर्शों की प्रतिष्ठापना का एक सशक्त माध्यम हैं। इसमें सन्निहित विचार प्रवाह में मनुष्य को श्रेष्ठ, उदार एवं उदात्त बनाने के सारे तत्व विद्यमान हैं। ऐसे किसी दर्शन की खोज करनी हो जो विवादों से रहित एवं बोधगम्य हो तो वह यज्ञदर्शन ही हो सकता है।’’ (अखण्ड ज्योति, सितम्बर १९८१, पृष्ठ ४७)। वे लिखते हैं कि ‘‘दान, देवपूजन और संगतिकरण का यज्ञीय दर्शन मनुष्य को उदार एवं उदात्त बनाने में हर दृष्टि से सक्षम है। इन तीनों सिद्धांतों में मानवी विकास के लिये असीम संभावनाएँ सन्निहित हैं। ’’ (उपरोक्त पृष्ठ ४९)
भगवान् श्रीकृष्ण ने इसी प्रकार यज्ञ की महत्ता बताते बताते अपने कथन की पूर्णता इन शब्दों में व्यक्त कर दी है कि जो यज्ञावशिष्ट अमृत का भोग करते हैं, वे ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं (यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्)। वे कह जाते हैं कि यज्ञ ही विश्व का विधान है, यज्ञ के बिना जीवन ही नहीं- पारलौकिक जीवन में भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। न लोक में प्रभुत्व मिल सकता है, न परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद वे कह जाते हैं कि ‘‘ब्रह्म के मुख में अर्थात् वेद की वाणी में इस प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं। उन सबको तू कर्म से अर्थात् मन इन्द्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा उत्पन्न जानना। किंतु यह भी जान ले कि परमात्मा कर्मादि से परे है- ऐसा जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो सकेगा।’’ (श्लोक ३२ का भावार्थ)
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ४/३२
इकत्तीसवें श्लोक की पराकाष्ठा के रूप में मुक्ति के राजमार्ग- इस बत्तीसवें श्लोक में देखने को मिलती है। ये सभी यज्ञ जो ऊपर बताए गए भगवान् विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण के अनुसार ब्रह्मा के मुख से निःसृत हुए हैं- उस अग्रि के मुख से जो सभी द्रव्यों को ग्रहण करती है। सर्वव्यापी ब्रह्म की सदायज्ञों में प्रतिष्ठित है। संसार के सभी प्रकार के कर्म परम पिता परमात्मा के उद्देश्य से अर्पित यज्ञ बन सकते हैं। यदि हम भोजन करें तो यह मानकर करें कि ब्रह्म को आहुति दे रहे हैं- जगज्जननी महाकाली को भोजन करा रहे हैं। यदि मार्ग पर चल रहे हों तो यह भावना करें कि जगन्माता की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक ये तीनों प्रकार के कर्म जब प्रभु की प्रसन्नता के लिये, ईश्वर में अर्पण बुद्धि से किये जायें तो सभी कर्मयज्ञ में परिणित हो जाते हैं। ऐसे यज्ञों का प्रतिफल पहले चित्त की शुद्धि तथा फिर आत्मोपलब्धि- जीवन्मुक्ति के रूप में मिलता है।
स्वामी विवेकानन्द ने इस विषय में काफी कुछ कहा है। गीता का कर्मयोग स्वामी जी के शब्दों में ‘‘वैज्ञानिक प्रणाली से किया गया एक कर्मानुष्ठान है। कर्मों का उद्देश्य है- मन के भीतर जो अन्तर्निहित शक्ति है- उसे प्रगट करना अर्थात् जीवात्मा का जागरण करना। जो कुछ करो- जो कुछ खाओ- जो कुछ हवन करो- जो कुछ तप करो- जो कुछ दो सभी मुझ भगवान् में अर्पण कर शान्तभाव से स्थित होकर रहो।’’
स्वामी जी जिस भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं- उसी का बोध श्रीकृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कराते हुए उसकी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सभी साधनों या यज्ञों को कर्मज मान- कर्म से जन्मा मान पर यह भी समझ कि ये सभी एक भगवान् की विशाल शक्ति से जन्मे हैं, उसी के द्वारा निर्दिष्ट हैं। उस भगवान् तत्व को तत्व से जान कर भलीभाँति समझकर स्वयं को समर्पित कर यज्ञीय भाव से यदि हर कर्म किया जाएगा तो लोभ- मोह के भवबंधनों से हमेशा के लिये जीवन्मुक्ति मिल जाएगी। (एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे)
गीताकार के काव्य का सौन्दर्य उसके शब्दों के गुंथन से बढ़कर उसके भावों की निरन्तर उच्चतर- उच्चतम सोपान पर चलते जाने के क्रम में दिखाई पड़ता है। यदि हम यह मर्म जान लें कि हमें कर्म क्यों करना है, किसके लिये करना है, यज्ञीय भाव से किये गये कर्म क्या होते हैं एवं जीवन को यदि बंधनों में बंधने से बचाकर मुक्ति का पथ प्रशस्त कैसे करना है तो हम जीवन दर्शन जान लेते हैं। इसी बात को भगवान् आगे बढ़ाते हुए तैतीसवें श्लोक में द्रव्यमय यज्ञ के रूप में सबसे नीची सीढ़ी एवं ज्ञानमय यज्ञ के रूप में सबसे ऊँची सीढ़ी बताते हैं।
Versions
-
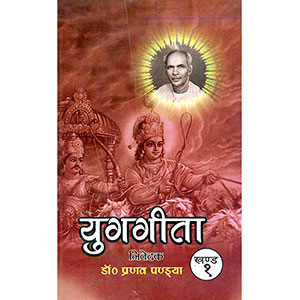
HINDIयुग गीता (भाग-1)Scan Book Version
-
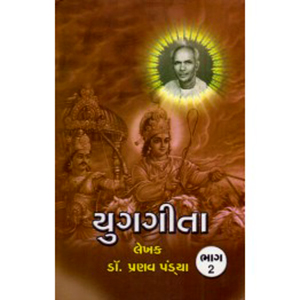
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૨Scan Book Version
-
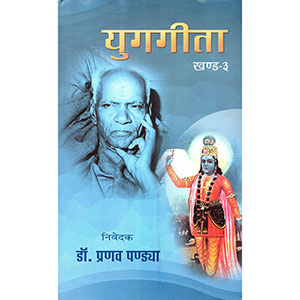
HINDIयुगगीता (भाग-३)Text Book Version
-
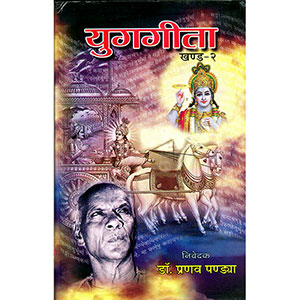
HINDIयुगगीता - (भाग-२)Text Book Version
-
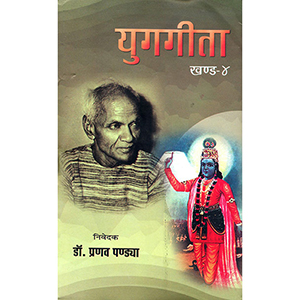
HINDIयुगगीता (भाग-४)Text Book Version
-
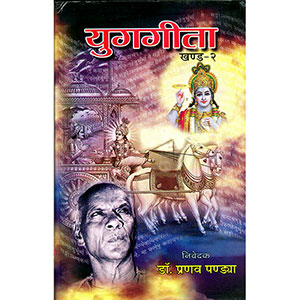
HINDIयुग गीता भाग-2Scan Book Version
-
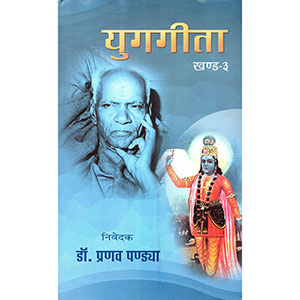
HINDIयुग गीता भाग-3Scan Book Version
-
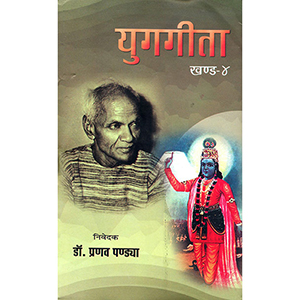
HINDIयुग गीता भाग-4Scan Book Version
-
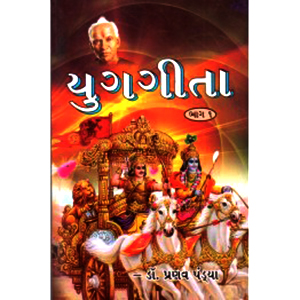
GUJRATIયુગગીતા ભાગ - ૧Scan Book Version
Write Your Comments Here:
- प्रथम खण्ड की प्रस्तावना
- प्रस्तुत द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना
- मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और किसलिए आए हो?
- धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
- जन्म कर्म च मे दिव्यम्
- वीतराग होने पर प्रभु के स्वरूप को प्राप्त होना
- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
- कर्म, अकर्म तथा विकर्म
- कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का मर्म
- गहना कर्मणोगति
- कैसे बनें दिव्यकर्मी और कैसे हों बंधनमुक्त
- कर्म में ब्रह्मदर्शन से ब्रह्म की ही प्राप्ति
- हर श्वास में संपादित दिव्य कर्म ही हैं यज्ञ
- यज्ञ बिना यह लोक नहीं तो परलोक कैसा?
- यज्ञों में श्रेष्ठतम-ज्ञानयज्ञ
- ज्ञान की नौका से भवसागर को पार करें
- पूर्ण तृप्त ज्ञानी की परिणति
- उठो भारत स्वयं को योग में प्रतिष्ठित करो

