गायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग) 
अनादि गुरु मंत्र गायत्री
Read Scan Versionमनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जहां कितनी ही विशेषताएं हैं वहां कितनी ही कमियां भी हैं। एक सबसे बड़ी कमी यह है कि पशु पक्षियों के बच्चे बिना किसी के सिखाये अपनी जीवन चर्या की साधारण बातें अपने आप सीख जाते हैं पर मनुष्य का बालक ऐसा नहीं करता है, यदि उसका शिक्षण दूसरों के द्वारा न हो तो वह उन विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य में होती हैं।
अभी कुछ दिन पूर्व की बात है दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में एक मादा भेड़िया मनुष्य के दो छोटे बच्चों को उठा ले गई। कुछ ऐसी विचित्र बात हुई कि उसने उन्हें खाने की बजाय अपना दूध पिला कर पाल लिया। वे बड़े हो गये। एक दिन शिकारियों का एक दल भेड़ियों की तलाश में उधर से निकला तो हिंसक पशुओं की मांद में मनुष्य के बालक देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उन्हें पकड़ जाये। ये बालक भेड़ियों की तरह चलते थे, वैसे ही गुर्राते थे वही सब खाते थे और उनकी सारी मानसिक स्थिति भेड़ियों जैसी थी। कारण यही था कि उन्होंने जैसा देखा वैसा सीखा और वैसे ही बन गये।
जो बालक जन्म से बहरे होते हैं वे जीवन भर गूंगे भी रहते हैं। क्योंकि बालक दूसरों के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर उनकी नकल करना सीखता है। यदि कान बहरे होने की वजह से वह दूसरों के शब्द सुन नहीं सकता तो फिर यह असम्भव है कि वह शब्दोच्चारण कर सके धर्म संस्कृति, रिवाज, भाषा, वेष भूषा, शिष्टाचार, आहार विहार, आदि बातें बालक अपने निकटवर्ती लोगों से सीखता है। यदि कोई बालक जन्म से ही अकेला रखा जाय तो वह उन सब बातों से वंचित रह जायगा जो मनुष्य में होती हैं।
पशु पक्षियों के बच्चों में यह बात नहीं है। बया पक्षी का छोटा बच्चा पकड़ लिया जाय और वह मां बाप से कुछ न सीखे तो भी बड़ा होकर अपने लिए वैसा ही सुन्दर घोंसला बना लेगा जैसा कि अन्य बया पक्षी बनाते हैं। पर अकेला रहने वाला मनुष्य का बालक भाषा, कृषि, शिल्प, संस्कृति, धर्म, शिष्टाचार, लोक व्यवहार श्रम, उत्पादन आदि सभी बातों से वंचित रह जायगा। पशुओं के बालक जन्मते ही चलने फिरने लगते हैं और माता का पय पान करने लगते हैं पर मनुष्य का बालक बहुत दिन में कुछ समझ पाता है। आरम्भ में तो वह करवट बदलना दूध का स्थान तलाश करना तक नहीं जानता, अपनी माता तक को नहीं पहचानता। इन बातों में पशुओं के बच्चे अधिक चतुर होते हैं।
मनुष्य कोरे कागज के समान है, कागज पर जैसी स्याही से जैसे अक्षर बनाये जाते हैं वैसे बन जाते हैं। फोटोग्राफी के प्लेट पर जैसी छाया पड़ती है वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है। मानव मस्तिष्क की रचना भी कोरे कागज एवं फोटो-प्लेट की भांति है। वह निकटवर्ती वातावरण में से अनेक बातें सीखता है। उसके ऊपर जिन बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है उन्हें वह अपने मानस क्षेत्र में जमा कर लेता है। मनुष्य गीली मिट्टी के समान है उसे जैसे सांचे में ढाल दिया जाय वैसा ही खिलौना बन जाता है। उच्च परिवारों में पलने वाले बालकों में वैसी विशेषताएं होती हैं और निकृष्ट श्रेणी के बीच रहकर जो बालक पलते हैं उनमें वैसी क्षुद्रताएं बहुधा पाई जाती हैं।
हमारे पारदर्शी पूर्वज, मनुष्य का इस कमजोरी को भरी प्रकार समझते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यदि बालकों पर अनियंत्रित प्रभाव पड़ता रहा, उसमें सुधार और परिवर्तन का प्रारम्भ से ही ध्यान न रखा गया तो यह बहुत मुश्किल है कि वे अपनी मनोभूमि को वैसा बना सकें जैसा कि मानस प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। आमतौर से सब माता पिता उतने सुसंस्कृत नहीं होते कि अपने बच्चों पर केवल अच्छा प्रभाव ही पड़ने दें और बुरे प्रभाव से उन्हें बचाते रहें। दूसरे यह भी है कि मां बाप में बालक के प्रति लाड़ प्यार स्वभावतः अधिक होता है, वे उनके प्रति अधिक उदार एवं मोह ग्रस्त होते हैं ऐसी दशा में अपने बालकों की बुराइयां उन्हें सूझ भी नहीं पड़ती। फिर इतने सूक्ष्मदर्शी मां बाप भी कहां होते हैं जो अपनी संतान की मानसिक स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण करके कुसंस्कारों का परिमार्जन तत्काल करने को उद्यत रहें।
सत् शिक्षण की आवश्यकता :—
मनुष्य की यह कमजोरी कि वह दूसरों से ही सब कुछ सीखता है, उसके उच्च विकास में बाधक होती है। कारण कि साधारण वातावरण में भले तत्वों की अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते हैं। उन बुरे तत्वों में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी से खिंच जाते हैं। फल स्वरूप वे बुराइयां अधिक सीख लेने के कारण आगे चलकर बुरे मनुष्य साबित होते हैं। छोटी आयु में यह पता नहीं चलता कि बालक किन संस्कारों को अपनी मनोभूमि में जमा रहा है, बड़ा होने पर जब वे संस्कार एवं स्वभाव प्रकट होते हैं तब उन्हें हटाना कठिन हो जाता है क्योंकि दीर्घकाल तक वे संस्कार बालक के मन में जमे रहने एवं पकते रहने के कारण ऐसे सुदृढ़ हो जाते हैं कि उनका हटाना कठिन होता है।
ऋषियों ने इस भारी कठिनाई को देख कर एक अत्यन्त ही सुन्दर और महत्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर मां बाप के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियंत्रण रहना चाहिये जो मनोविज्ञान को सूक्ष्मताओं को समझता हो, दूरदर्शी, तत्वज्ञानी और पारदर्शी होने के कारण बालक के मन में जमते रहने वाले संस्कार बीजों को अपनी पैनी दृष्टि से तत्काल देख लेने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता रखता हो। ऐसे मानसिक नियंत्रण कर्ता की उनने प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य आवश्यकता घोषित की।
शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के तीन प्रत्यक्ष देव हैं (1) माता (2) पिता (3) गुरु। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपमा दी है। माता जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा है, पिता पालन करता है इसलिए विष्णु है, गुरु कुसंस्कारों का संहार करता है इसलिए शंकर है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष है। कोई यह कहे कि मैं बिना माता के पैदा हुआ तो उसे झूठा कहा जायगा क्योंकि बिना माता के गर्भ में रहे, भला कोई किस प्रकार जन्म ले सकता है? इसी प्रकार कोई यह कहे कि मैं बिना बाप का हूं। तो उसे ‘वर्णशंकर’ कहा जायगा क्योंकि जिसके बाप का पता न हो ऐसे बच्चे तो वेश्याओं के यहां ही पैदा होते हैं। उसी प्रकार कोई कहे कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो समझा जायगा कि यह असभ्य एवं असंस्कारित है। क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर विचार, स्वभाव, ज्ञान, गुण, कर्म आदि पर किसी दूरदर्शी का नियंत्रण नहीं रहा उसके मानसिक स्वस्थता का क्या भरोसा किया जा सकता है? ऐसे असंस्कृत व्यक्तियों को ‘निगुरा’ कहा जाता है। ‘निगुरा’ का अर्थ है—बिना गुरु का। किसी समय में ‘निगुरा’ कहना भी ‘वर्णशंकर’ या ‘मथ्याचारी’ कहलाने के समान गाली समझी जाती थी।
बिना माता का, बिना पिता का, बिना गुरु का, भी कोई मनुष्य हो सकता है यह बात प्राचीन काल में अविश्वस्त समझी जाती थी। कारण कि भारतीय समाज के सुसंबद्ध विकास के लिए ऋषियों की यह अनिवार्य व्यवस्था थी कि प्रत्येक आर्य का गुरु होना चाहिए। जिससे वह महान पुरुष बन सके। उस समय प्रत्येक माता पिता को अपने बालकों को महापुरुष बनाने की अभिलाषा रहती थी। इसके लिए यह आवश्यकता थी कि उनके बालक किसी सुविज्ञ आचार्य के शिष्य हों।
गुरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था। पढ़ने की आयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रम में भेज दिये जाते थे। राजा महाराजाओं तक के बालक गुरुकुलों का कठोर जीवन बिताने जाते थे ताकि वे कुशल नियंत्रण में रहकर सुसंस्कृत बन सकें और आगे चलकर मनुष्यता के महान गौरव की रक्षा करने वाले महापुरुष सिद्ध हो सकें। ‘मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूं।’ यह बात बड़े गौरव के साथ कही जाती थी। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे को अपना परिचय देता था तो कहता था ‘‘मैं अमुक आचार्य का शिष्य, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गौत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति हूं।’’ संकल्पों में, प्रतिज्ञाओं में, साक्षी में, राज दरबार में, अपना परिचय इसी आधार पर दिया जाता था।
मनोभूमि का परिष्कार :—
बगीचे को यदि सुन्दर बनाना है तो उसके लिये किसी कुशल माली की नियुक्ति आवश्यक है। जब आवश्यकता हो तब सींचना, जब अधिक पानी भर गया हो तो उसे बाहर निकाल देना, समय पर गोड़ना, निराई करना, अनावश्यक टहनियों को छांटना, खाद देना, पशुओं को चरने न देने की रखवाली करना आदि बातों के सम्बन्ध में माली सदा सजग रहता है, फल स्वरूप वह बगीचा हरा भरा, फला फूला सुन्दर और समुन्नत रहता है।
मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचा है, इसमें नाना प्रकार के मनोभाव, विचार, संकल्प, इच्छा, वासना, योजना रूपी वृक्ष उगते हैं उनमें से कितने ही आवश्यक और कितने ही अनावश्यक होते हैं। बगीचे में कितने ही पौधे झाड़ झंखाड़ के अपने आप उग आते हैं, वे बढ़ें तो बगीचे को नष्ट कर सकते हैं इसलिए माली उन्हें उखाड़ देता है और दूर दूर से लाकर अच्छे अच्छे बीज उसमें बोता है। गुरु अपने शिष्य के मस्तिष्क रूपी बगीचे का माली होता है वह अपने क्षेत्र में से जंगली झाड़ झंखाड़ जैसे अनावश्यक संकल्पों संस्कारों, आकर्षणों और प्रभावों को उखाड़ता रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं चतुरता के साथ ऐसे संस्कार बीज जमाता रहता है जो उस मस्तिष्क रूपी बगीचे को बहुमूल्य बनावें।
कोई व्यक्ति यह सोचे कि ‘‘मैं स्वयं ही अपना आत्म-निर्माण करूंगा, अपने आप अपने को सुसंस्कृत बनाऊंगा मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं।’’ तो ऐसा किया जा सकता है। आत्मा में अनन्त शक्ति है। अपना कल्याण करने की शक्ति इसमें मौजूद है। परन्तु ऐसे प्रयत्नों में कोई मनस्वी व्यक्ति ही सफल होते हैं। सर्व साधारण के लिये यह बात बहुत कष्ट साध्य है। क्योंकि बहुधा अपने दोष अपने को नहीं दीखते, अपनी आंखें अपने आपको स्वयं दिखाई नहीं देतीं। किसी दूसरे मनुष्य या दर्पण की सहायता से ही अपनी आंखों को देखा जा सकता है। जब कोई वैद्य डॉक्टर बीमार होते हैं तो स्वयं अपना इलाज आप नहीं करते क्योंकि अपनी नाड़ी स्वयं देखना, अपना निदान आप कर लेना साधारण तथा बहुत कठिन होता है इसलिए वे किसी दूसरे वैद्य डॉक्टर से अपनी चिकित्सा कराते हैं।
कई सुयोग्य व्यक्ति भी आत्म निरीक्षण में सफल नहीं होते। हम दूसरों की जैसी अच्छी आलोचना कर सकते हैं, दूसरों को जैसी नेक सलाह दे सकते हैं वैसी अपने लिए नहीं कर पाते। कारण यही है कि अपने सम्बन्ध में आप निर्णय करना कठिन होता है। कोई अपराधी ऐसा नहीं जिसे यदि मजिस्ट्रेट बना दिया जाय तो अपने अपराध के सम्बन्ध में उचित फैसला ले सके। निष्पक्ष फैसला कराना हो तो किसी दूसरे जज का आश्रय लेना पड़ेगा। आत्म निर्माण का कार्य भी ऐसा ही है जिसके लिए दूसरे सुयोग्य सहायक की गुरु की आवश्यकता होती है।
समुचित बौद्धिक विकास की सुव्यवस्था के लिए ‘गुरु’ की नियुक्ति को भारतीय धर्म में आवश्यक माना गया है। जिससे मनुष्य की विचारधारा, स्वभाव, संस्कार, गुण, प्रकृति, आदतें, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कार्य पद्धति आदि का प्रवाह उत्तम दिशा में हो और मनुष्य अपने आप में संतुष्ट प्रसन्न, पवित्र और परिश्रमी रहे एवं दूसरों को अपनी उदारता तथा सद्व्यवहार से सुख पहुंचावे। इस प्रकार के सुसंस्कृत मनुष्य जिस समाज में, जिस देश में, अधिक होंगे वहां निश्चय पूर्वक सुख शान्ति की, सुव्यवस्था की, पारस्परिक सहयोग की, प्रेम की, साथ ही सहयोग की बहुलता रहेगी। हमारा पूर्व इतिहास साक्षी है कि सुसंस्कारित मस्तिष्क के भारतीय महापुरुषों ने कैसे महान कार्य किये थे, और इस भूमि पर किस प्रकार स्वर्ग को अवतरित कर दिया था।
हमारे पूर्व कालीन महान् गौरव की नींव में ऋषियों की दूरदर्शिता छिपी हुई थी जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपना मानसिक परिष्कार कराने के लिए किसी उच्च चरित्र, आदर्शवादी, सूक्ष्मदर्शी, विद्वान के नियंत्रण में रहना आवश्यक होता था जो व्यक्ति मानसिक परिष्कार कराने की आवश्यकता से जी चुराते थे उन्हें ‘निगुरा’ की गाली दी जाती थी ‘निगुरा’ शब्द का अपमान करीब करीब ‘बिना बाप का’ या ‘वर्ण शंकर’ कहे जाने के बराबर समझा जाता था। धन कमाना, विद्या पढ़ाना, शस्त्र चलाना, सभी बातें आवश्यक थीं पर मानसिक परिष्कार तो सबसे अधिक आवश्यक था। क्योंकि असंस्कृत मनुष्य तो समाज का अभिशाप बनकर ही रहता है भले ही उसके पास कितनी ही अधिक भौतिक सम्पदा क्यों न हो। गुरु को प्रत्यक्ष तीन देवों में तीन परम पूज्यों में स्थान देने का यही कारण था।
दूषित वातावरण का प्रभाव :—
आज वह प्रथा टूट चली है। गुरु कहलाने के अधिकारी व्यक्तियों का मिलना मुश्किल है। जिनमें गुरु बनने की योग्यता है वे अपने व्यक्तिगत आत्मिक या भौतिक लाभों के संपादन में लगे हुए हैं। लोक सेवा एवं राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर, सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व शिर पर लेने की ओर उनका ध्यान नहीं है। वे इससे स्वल्प लाभ, अधिक झंझट और भारी बोझ अनुभव करते हैं। इसकी अपेक्षा वे दूसरे सरल तरीकों से अधिक धन और यश कमा लेने के अनेक मार्ग जब सामने देखते हैं तो ‘गुरु’ का गहन उत्तरदायित्व ओढ़ने से कन्नी काट जाते हैं।
दूसरी ओर, ऐसे अयोग्य व्यक्ति जितना चरित्र, ज्ञान, अनुभव, विवेक, तप आदि कुछ भी नहीं है जिनमें दूसरों को संस्कृत करने की क्षमता होना तो दूर जो अपने आपको सुसंस्कृत नहीं बना सके, जो अपना निर्माण नहीं कर सके ऐसे लोग पैर पुजाने और दक्षिणा लेने के लोभ में कान फूंकने लगे, खुशामद दीनता और भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर शिष्य तलाश करने लगे तो गुरुत्व की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। जिस काम को कुपात्र लोग हाथ में ले लेते हैं वह अच्छा काम भी बदनाम हो जाता है और जिस साधारण काम को यदि भले व्यक्ति करने लगें तो वह अच्छा हो जाता है। दीन दुखियों के हाथ में रहने से चरखा चखाना ‘दुर्भाग्य’ का चिन्ह समझा जाता था पर गांधी जी जैसे महापुरुष के हाथ पहुंच कर वही चरखा यज्ञ बन जाता है। ऋषियों के हाथ में जब तक ‘गुरुत्व’ था तब तक उस पद की प्रतिष्ठा रही आज जब कि कुपात्र, भिखारी और क्षुद्र लोग गुरु बनने का दुस्साहस करने लगे तो वह महान पद ही बदनाम हो गया। आज ‘गुरु’ या ‘गुरु घंटाल’ शब्द किसी पुराने पापी या धूर्त राज के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
लोगों ने देखा कि एक आदमी दक्षिणा भी लेता है पैर भी पुजवाता है पर वह किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंचाता तो उनने भी इस व्यर्थ के झंझट को तोड़ देना उचित समझा। गुरु शिष्य की परम्परा शिथिल होने लगी और धीरे धीरे उसका लोप होने लगा। ठीक भी है निष्प्रयोजन, निष्प्राण, निरुपयोगी, होने पर भी जो परम्पराएं खर्चीली है वे देर तक जीवित नहीं रह सकतीं। अब बहुत कम मनुष्य ऐसे रह गये हैं जो गुरु की नियुक्ति आवश्यक समझते हों, या ‘निगुरा, कहलाने में अपना अपमान समझते हों।
आज के दूषित वातावरण ने सभी दिशाओं में गड़बड़ी पैदा कर दी है। असली सोना कम है पर नकली सोना बेहिसाब तैयार हो रहा है। असली घी मिलना मुश्किल है पर वेजीटेबल घी से दुकानें पटी पड़ी हैं। असली मोती, असली जवाहरात कम हैं पर नकली मोती, और इमीटेशन रत्न ढेरों बिकते हैं। इतना होते हुए भी असली चीजों का महत्व कम नहीं हुआ है। लोग घासलेट घी को खूब खरीदते बेचते हैं पर इससे असली घी की उपयोगिता घट नहीं जाती। असंख्य गड़बड़ियां होते रहने पर भी असली घी के गुण वही रहेंगे और उसके लाभों में कोई कमी न होगी। असली सोना, असली रत्न, आदि भी इसलिए निरुपयोगी नहीं हो जाते कि नकली चीजों ने उस क्षेत्र को बदनाम कर दिया है। मिलावट, नकली पन धोखाधड़ी के हजार पर्वत मिलकर भी वास्तविकता, वस्तु स्थिति का, महत्व राई भर भी नहीं घटा सकते।
‘‘व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति का निर्माण’’ एक सचाई है, जो आज की विषम स्थिति में तो क्या, किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में भी गलत सिद्ध नहीं हो सकती। रोटी बनानी होगी तो आटे की, पानी की, आग की, जरूरत पड़ेगी। चाहे कैसा ही भला या बुरा समय हो इस अनिवार्य आवश्यकता में कोई अन्तर नहीं आ सकता। अच्छे मनुष्य, सच्चे मनुष्य, प्रतिष्ठित मनुष्य, सुखी मनुष्य की रचना के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे सुयोग्य और दूरदर्शी मनुष्यों द्वारा हमारे मस्तिष्कों का नियंत्रण, संशोधन, निर्माण और विकास किया जाय। मनुष्य कोरे कागज के समान है वह जैसा प्रभाव ग्रहण करेगा, जैसा सीखेगा, वैसा करेगा। यदि बुराई से बचना है तो अच्छाई से सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक है। मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकता, उसे अच्छाई का प्रकाश न मिलेगा तो निश्चय ही उसे बुराई के अन्धकार में रहना होगा।
शिक्षा और विद्या का महत्व :—
मनुष्य को सुयोग्य बनाने के लिए उसके मस्तिष्क को दो प्रकार से उन्नत किया जाता है (1) शिक्षा द्वारा (2) विद्या द्वारा। शिक्षा के अन्तर्गत वे सब बातें आती हैं जो स्कूलों में कालेजों में, ट्रेनिंग कैम्पों में हाट बाजार में, घर में, दुकान में, समाज में सिखाई जाती हैं। गणित, भूगोल, इतिहास भाषा, शिल्प, व्यायाम, रसायन, चिकित्सा, निर्माण, व्यापार, कृषि, संगीत, कला, आदि बातें सीखकर मनुष्य व्यवहार कुशल, चतुर, कमाऊ, लोक प्रिय एवं शक्ति सम्पन्न बनता है। विद्या द्वारा मनोभूमि का निर्माण होता है। मनुष्य की इच्छा आकांक्षा, भावना, श्रद्धा, मान्यता, रुचि, एवं आदतों के अच्छे ढांचे में ढालना विद्या का काम है। चौरासी लाख योनियों में घूमते हुए आने के कारण पिछले पाशविक संस्कारों से मन भरा रहता है उनका संशोधन करना विद्या का काम है।
शिक्षक ,शिक्षा देता है। शिक्षा का अर्थ है—सांसारिक ज्ञान। विद्या का अर्थ है—मनोभूमि की सुव्यवस्था। शिक्षा आवश्यक है, पर विद्या उससे भी अधिक आवश्यक है। शिक्षा बढ़नी चाहिए, पर विद्या का विस्तार उससे भी अधिक होना चाहिए। अन्यथा दूषित मनोभूमि रहते हुए यदि सांसारिक सामर्थ्यं बढ़ीं तो उसका परिणाम भयंकर होगा। धन की, चतुरता की, शिक्षा की, विज्ञान की, इन दिनों बहुत उन्नति हुई है पर यह स्पष्ट है कि उन्नति के साथ साथ हम सर्वनाश की ओर ही बढ़ रहे हैं कम साधन होते हुए भी कम शिक्षा होते हुए भी, विद्यावान् मनुष्य सुखी रह सकता है परन्तु केवल बौद्धिक या सांसारिक शक्तियां होने पर दूषित मनोभूमि का मनुष्य अपने लिए तथा दूसरों के लिए केवल विपत्ति, चिन्ता, कठिनाई क्लेश एवं बुराई ही उत्पन्न कर सकता है। इसलिए विद्या पर भी उतना ही बल्कि उससे भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए जितना कि शिक्षा पर दिया जाता है।
आज हम अपने बालकों को ग्रेजुएट बना देने के लिए ढेरों पैसा खर्च करते हैं पर उनकी आन्तरिक भूमिका को सुव्यवस्थित करने की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं करते, फलस्वरूप ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी वे बालक अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति कोई आदर्श व्यवहार नहीं कर पाते। किसी भी ओर उनकी प्रगति ऐसी नहीं होती जो प्रसन्नता दायक हो। शिक्षा के साथ उनमें जो अनेक दुर्गुण आ जाते हैं उन दुर्गुणों में ही उनकी योग्यता द्वारा होने वाली कमाई बर्बाद होती रहती है।
इस तथ्य को हमारे पूर्वज जानते थे कि शिक्षा से भी, विद्या का महत्व अधिक है। इसलिए वे छोटी ही आयु में अपने बच्चों पर गुरु का नियंत्रण स्थापित करा देते थे। गुरु लोग अपने गम्भीर ज्ञान, विशाल अनुभव, सूक्ष्मदर्शी विवेक और निर्मल चरित्र द्वारा शिष्य को प्रभावित करके उसकी मनोभूमि का निर्माण करते थे। अपनी प्रचण्ड शक्ति किरणों द्वारा उसके अन्तःकरण में ऐसे बीज अंकुरित कर देते थे जो फलने फूलने पर उस व्यक्ति को महापुरुष सिद्ध करें।
गायत्री द्वारा द्विजत्व की प्राप्ति :—
भारतीय धर्म के अनुसार, गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय के लिए है। जैसे ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति भारतीय आचार के प्रति, ऋषियों और देवताओं के प्रति आस्था एवं आदर बुद्धि का होना भारतीय धर्म के अनुयायी के लिए आवश्यक है वैसे ही यह आवश्यक है कि वह ‘निगुरा’ न हो। उसे किसी सुयोग्य सत्पुरुष का ऐसा पथ प्रदर्शन प्राप्त होना चाहिए जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके।
संभ्रान्त भारतीय धर्मानुयायी को ‘द्विज’ कहते हैं। द्विज वह है जिसका दो बार जन्म हुआ है। एक बार माता पिता के रज वीर्य से सभी का जन्म होता है। इस तरह मनुष्य जन्म पा लेने से कोई मनुष्य प्रतिष्ठित आर्य नहीं बन सकता। केवल जन्म मात्र से मनुष्य का कोई गौरव नहीं कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पशुओं से भी गये बीते होते हैं। स्वभावतः जन्म जात पशुता तो प्रायः सभी में होती है इस पशुता का मनोविज्ञान परिष्कार किया जाता है उस परिष्कार की पद्धति को द्विजत्व या दूसरा जन्म कहते हैं।
शास्त्र में बताया गया है कि—‘‘जन्मनां जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चते।’’ अर्थात् जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। संस्कारों द्वारा, प्रभावों द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, यह दूसरा जन्म माता गायत्री और पिता आचार्य द्वारा होता है। गायत्री के 24 अक्षरों में ऐसे सिद्धान्त और आदर्श सन्निहित हैं जो मानव अन्तःकरण को उच्च स्तर पर विकसित करने के प्रधान आधार हैं। समस्त वेद शास्त्र पुराण, स्मृति, उपनिषद् आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र आदि ग्रन्थों में जो कुछ भी शिक्षा है वह गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं की व्याख्या मात्र है। समस्त भारतीय धर्म, समस्त भारतीय आदर्श, समस्त भारतीय संस्कृति का सर्वस्व गायत्री के 24 अक्षरों में बीज रूप से मौजूद है। इसलिए द्विजत्व के लिए, दूसरे जन्म के लिए, गायत्री को माता माना गया है।
चूंकि वे शिक्षाएं केवल मंत्र याद कर लेने या पुस्तकों में लिखी हुई बातें पढ़ लेने मात्र से हृदयंगम नहीं हो सकती। पढ़ने से किसी बात की जानकारी तो हो जाती है पर हृदय में उनको प्रवेश करा देना किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा ही हो सकता है दीपक को दीपक से जलाया जाता है, अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, सांचे में वस्तुएं ढाली जाती हैं, व्यक्तियों से व्यक्तियों का निर्माण होता है। इसलिए गायत्री की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में जीवन में घुला देने का कार्य न तो अपने आप किया जा सकता है और न उसके पढ़ने मात्र से होता है, उसके लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। दूसरे जन्म का, द्विजत्व का, आदर्श जीवन का, पिता गुरु को माना गया है।
गुरु द्वारा गायत्री के आधार पर जो शिक्षाएं दी जाती हैं उनको भली प्रकार हृदयंगम करने, सदा छाती से चिपटाये रहने, उनका पूरी तरह प्रयोग करने का उत्तर दायित्व कंधे पर रखा हुआ अनुभव करने की बात हर समय आंखों के आगे रहे, इसके लिए द्विजत्व का प्रतीक यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री में नौ पद हैं 1-तत् 2-सवितुः 3-वरेण्यं 4-भर्गो 5-देवस्य 6-धीमहि 7-धियो 8-योनः 9-प्रचोदयात् यज्ञोपवीत में नौ धागे हैं। प्रत्येक धागा गायत्री के एक एक पद का प्रतीक है। यज्ञोपवीत में तीन ग्रन्थियां और एक अन्तिम ब्रह्म ग्रन्थि होती है। बड़ी ग्रन्थि गायत्री के ‘ॐ’ की, और शेष तीन गाठें भूः भुवः स्वः की प्रतीक हैं। जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा की जाती है वैसे ही गायत्री की मूर्ति सूत की बना कर हृदय मन्दिर पर प्रतिष्ठित की जाती है। मन्दिर की मूर्ति के सम्मुख हर घड़ी नहीं रहा जा सकता पर गायत्री की प्रतिमा का तो, यज्ञोपवीत का तो, हर घड़ी पास रहना आवश्यक है, उसे तो क्षण भर के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता। वह तो हर घड़ी हृदय के ऊपर झूलता रहता है, उसका बोझ तो हर घड़ी कन्धे पर रखा रहता है। इस प्रकार गायत्री पूजा को, गायत्री की प्रतिमा को, गायत्री की शिक्षा को, जीवन संगिनी बनाया गया है। कोई प्रतिष्ठित भारतीय धर्मानुयायी यज्ञोपवीत को छोड़ नहीं सकता, उसकी महत्ता से, आवश्यकता से, इनकार कर नहीं सकता।
कहा जाता है गायत्री का अधिकार केवल द्विजों का है। द्विजत्व का तात्पर्य है—गुरु द्वारा गायत्री को ग्रहण करना। जो लोग अश्रद्धालु हैं, आत्म निर्माण से जी चुराते हैं, आदर्श जीवन बिताने से उदासीन हैं, जिनकी सन्मार्ग में प्रवृत्ति नहीं, ऐसे लोग ‘शूद्र’ कहे जाते हैं। जो दूसरे जन्म का आदर्श जीवन का, मनुष्यता की महानता का, सन्मार्ग का, अवलम्बन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों का जन्म पाशविक ही कहा जायगा। ऐसे लोग गायत्री में क्या रुचि लेंगे? जिसकी जिस मार्ग में श्रद्धा न होगी वह उसमें क्या सफलता प्राप्त करेगा? इसलिए ठीक ही कहा गया है कि शूद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं, इस महा विद्या का अधिकारी वही है जो आत्मिक कायाकल्प का लक्ष रखता है, जिसे पाशविक जीवन की अपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है, जो द्विज बनकर सैद्धान्तिक जन्म लेकर सत्पुरुष बनना चाहता है।
उत्कीलन और शाप मोचन :—
शास्त्रों में बताया गया है कि गायत्री मंत्र कीलित है, उसका जब तक उत्कीलन न हो जाय तब तक वह फल दायक नहीं होता। यह भी कहा गया है कि गायत्री को शाप लगा हुआ है। उस शाप का जब तक ‘अभिमोचन’ न कर लिया जाय तब तक उससे कुछ लाभ नहीं होता। कीलित होने और शाप लगने के प्रतिबन्ध क्या हैं? और उत्कीलन एवं अभिमोचन क्या है? यह विचारणीय बातें हैं।
यह कहा जा सकता कि ‘‘औषधि विद्या कीलित है।’’ क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर शास्त्र निदान नघंटु, चिकित्सा विज्ञान की बारीकियों को नहीं समझता, अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी चिकित्सा आरम्भ करदे तो उससे कुछ भी लाभ न होगा, उलटी हानि हो सकती है। यदि औषधि से कोई लाभ लेना है तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ग्रन्थों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन्हें पढ़ कर बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं, फिर भी वैद्य की आवश्यकता तो है ही। वैद्य के बिना हजारों रुपये के चिकित्सा ग्रन्थ और लाखों रुपयों का औषधालय भी रोगी को कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकता। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ‘औषधि विद्या कीलित है।’ गायत्री महा विद्या के बारे में भी यही बात है। साधक की मनोभूमि के आधार पर साधना विधान में नियमोपनियमों में, आदर्शों में, ध्यान में, अनेक हेर फेर करने होते हैं। सबकी साधना एक-सी नहीं हो सकती, ऐसी दशा में उस व्यक्ति को पथ प्रदर्शन आवश्यक है जो इस विज्ञान का ज्ञाता एवं अनुभवी हो। जब तक ऐसा निर्देशक मिले तब तक औषधि विद्या की गायत्री विद्या भी साधक के लिए कीलित ही रहेगी। उपयुक्त निर्देशक का मिल जाना ही उत्कीलन है। ग्रन्थों में बताया है कि गुरु द्वारा ग्रहण कराई गई गायत्री ही उत्कीलित होती है। वही सफल होती है।
स्कंद पुराण में वर्णन है कि—एक बार वशिष्ठ, विश्वामित्र और ब्रह्मा ने क्रुद्ध होकर गायत्री को शाप दिया कि ‘‘उसकी साधना निष्फल होगी।’’ इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अन्त में ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो शाप मोचन की विधि को पूरा करके जो गायत्री की साधना करेगा उसका प्रयत्न तो सफल होगा और शेष लोगों का भ्रम निरर्थक जायगा। इस कथा में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है जिसे न जानने वाले केवल ‘‘शाप मुक्तोभव’’ वाले मंत्रों को पढ़ लेने मात्र से यह मान लेते हैं हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई।
विश्वामित्र का अर्थ है—संसार का मित्र, लोक सेवी परोपकारी। वशिष्ठ का अर्थ है—विशेष रूप से श्रेष्ठ। ब्रह्मा का अर्थ है—ब्रह्म परायण। इन तीन गुणों वाले पथ प्रदर्शक के आदेशानुसार होने वाले आध्यात्मिक प्रयत्न ही सफल एवं कल्याणकारी होते हैं।
स्वार्थी दूसरे का बुरा करने को उद्यत, वाम मार्गी मनोवृत्ति का मनुष्य यदि साधक को वैसी ही साधना सिखावेगा तो वह अपना और शिष्य का, दोनों का नाश करेगा। जिसका चरित्र उच्च नहीं, जो उदार नहीं, जिसमें महानता और प्रतिभा नहीं, वह दूसरों का क्या निर्माण करेगा? इसी प्रकार जो ब्रह्म परायण नहीं, जिसकी साधना एवं तपस्या नहीं, ऐसा गुरु किसी की आत्मा में क्या प्रकाश दे सकेगा? तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र-उदार, वशिष्ठ–महानता युक्त, ब्रह्मा-ब्रह्म परायण, इन तीनों गुणों से युक्त निर्देशक जब किसी व्यक्ति का निर्माण करेगा तो उसका प्रयत्न निष्फल नहीं जा सकता। इसके विपरीत कुपात्र, अयोग्य और अनुभव हीन व्यक्तियों की शिक्षानुसार की गई साधना तो इसी प्रकार व्यर्थ रहेगी मानो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर दिया हो! शाप लगने और उसके विमोचन करने का गुप्त रहस्य उपयुक्त मार्ग दर्शक की अध्यक्षता में अपनी कार्य पद्धति का निर्माण करना ही है।
गायत्री उच्च मानव जीवन की जन्मदात्री, आधार शिला, एवं बीज शक्ति है। भारतीय संस्कृति रूपी ज्ञान गंगा की उद्गम भूमि गंगोत्री यह गायत्री ही है, इसलिए इसे द्विजों की माता कहा गया है। माता के पेट में रहकर मनुष्य देही का जन्म होता है, गायत्री माता के पेट में रहकर मनुष्य का आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक, दिव्य विशेषताओं वाला, दूसरा जन्म होता है। परन्तु यह माता, सर्व सम्पन्न होते हुए भी पिता के अभाव में अपूर्ण हैं, द्विजत्व का दूसरा शरीर, माता और पिता दोनों के ही तत्व बिन्दुओं से निर्मित होता है। गायत्री माता की अदृश्य सत्ता को, गुरु द्वारा ही ठीक प्रकार से शिष्य की मनोभूमि में आरोपित किया जाता है। इसीलिए जब द्विजत्व का संस्कार होता है तो इस दूसरे आध्यात्मिक जन्म में गायत्री को माता और आचार्य को पिता घोषित किया जाता है।
उच्च आदर्शों की शिक्षा, न तो अपने आप प्राप्त हो जाती है न केवल आधार ग्रन्थों से। हीन चरित्र के अयोग्य व्यक्ति भी उन उच्च आदर्शों की ओर दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। बढ़िया धनुष बाण पास होते हुए भी कोई व्यक्ति शब्द वेधी बाण चलाने वाला नहीं बन सकता, और न अनाड़ी शिक्षक द्वारा बाण विद्या में पारंगत बना जा सकता है। अच्छा शिक्षक और अच्छा धनुष बाण दोनों मिलकर ही सफल परिणाम उपस्थित करते हैं। गायत्री के कीलित एवं शापित होने का और उसका उत्कीलन एवं शाप विमोचन करने का यही रहस्य है।
आत्म कल्याण की तीन कक्षाएं :—
आध्यात्मिक साधना क्षेत्र तीन भागों में बंटा हुआ है। तीन व्याहृतियों में उनका स्पष्टीकरण कर दिया है। (1) भूः (2) भुवः (3) स्वः यह तीन आत्मिक भूमिकाएं मानी गई हैं। भूः का अर्थ है स्थूल जीवन, शारीरिक एवं सांसारिक जीवन। भुः का अर्थ है—अन्तकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि चित्त, अहंकार का कार्य क्षेत्र। स्वः का अर्थ है—विशुद्ध आत्मिक सत्ता। मनुष्य की आन्तरिक स्थिति इन तीन क्षेत्रों में ही होती है।
‘‘भूः’’ का सम्बन्ध अन्नमय कोश से है। ‘‘भुवः’’ प्राणमय और मनोमय कोश से आच्छादित है। ‘‘स्वः’’ का प्रभाव क्षेत्र विज्ञानमय कोश और आनन्दमय कोश हैं। शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, जीविका उपार्जन, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नीति, शिल्प, कला स्कूली शिक्षा, व्यापार, सामाजिक राजनैतिक ज्ञान, नागरिक कर्तव्य आदि बातें भूःक्षेत्र में आती है। ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म, दर्शन, मनोबल, प्राण शक्ति, तांत्रिक प्रयोग, योग साधन, आदि बातें भुवः क्षेत्र की है। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर परायणता ब्राह्मी स्थिति, परमहंस गति समाधि, तुरीयावस्था, परमानन्द, मुक्ति का क्षेत्र ‘स्वः’ के अन्तर्गत हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के यह तीन लोक हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की भांति ही हमारे भीतर भूः भुवः स्वः तीन लोक है।
इन तीन स्थितियों के आधार पर ही गायत्री के तीन विभाग किये गये हैं। उसे त्रिपदी कहा गया है, उसके तीन चरण हैं। पहली भूमिका, प्रथम चरण, भूः क्षेत्र के लिए है। उसके अनुसार वे शिक्षाएं दी जाती हैं जो मनुष्य के व्यक्तिगत और सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने में सहायक होती है।
गायत्री गीता एवं गायत्री स्मृति में गायत्री के चौबीस अक्षरों की व्याख्या की गई है। एक एक अक्षर एवं शब्द से जिन सिद्धान्तों आदर्शों एवं उपदेशों की शिक्षा मिलती है वे इतने अमूल्य हैं कि उनके आधार पर जीवन नीति बनाने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य दिन दिन सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, एवं प्रतिष्ठा की ओर बढ़ता चला जाता है। गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में गायत्री कल्प वृक्ष का चित्र बनाकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि तत्, सवितुः, वरेण्यं, आदि अक्षरों का मनुष्य के लिए कैसा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शिक्षण है। वे शिक्षाएं अत्यन्त सरल, तत्काल अपना परिणाम दिखाने वाली, एवं घर बाहर सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने वाली हैं।
गायत्री की दस भुजाओं के सम्बन्ध में ‘‘गायत्री मंजरी’’ में यह बताया गया है कि इन दस भुजाओं से माता दस मूलों को नष्ट करती है। 1—दूषित दृष्टि 2—परावलंबन 3—भय 4—क्षुद्रता 5—असावधानी 6—स्वार्थ परता 7—अविवेक 8—आवेश 9—तृष्णा 10—आलस्य, यह दस शूल माने गये हैं। इन दस दोषों, मानसिक शत्रुओं को नष्ट करने के लिए 1 प्रथव ध्याहृति, तथा 9 पदों द्वारा दस ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दी गई हैं जो मानव जीवन में स्वर्गीय आनन्द की सृष्टि कर सकती हैं। नीति, धर्म, सदाचार, सम्पन्नता, व्यवहार, आदर्श, स्वार्थ और परमार्थ का जैसा सुन्दर समन्वय इन शिक्षाओं में है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। वेद शास्त्रों की सम्पूर्ण शिक्षाओं का निचोड़ इन अक्षरों में रख दिया गया है। इनका, जो जितना अनुसरण करता है वह तत्काल उतने ही अंशों में लाभान्वित हो जाता है।
प्रथम भूमिका मंत्र दीक्षा :—
जीवन का प्रथम चरण ‘भूः’ है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार में जो अनेकों गुत्थियां उलझनें, कठिनाइयां आती हैं उन सबका सुलझाव इन अक्षरों में दी हुई शिक्षा से होता है। सांसारिक जीवन का कोई भी कठिन प्रश्न ऐसा नहीं है, जिनका उत्तर और उपाय इन अक्षरों में न हो। इस रहस्यमय व्यवहारिक ज्ञान की आपके उपयुक्त व्याख्या कराने के लिए जिस गुरु की आवश्यकता होती है उसे ‘‘आचार्य’’ कहते हैं। आचार्य ‘मंत्र दीक्षा’ देते हैं। मंत्र का अर्थ है—विचार। तर्क, प्रमाण अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य अपने शिष्य को समय समय पर ऐसे सुझाव, सलाह, उपदेश, गायत्री मंत्र की शिक्षाओं के आधार पर देते हैं जिससे उसको उसकी विभिन्न समस्याओं का समाधान होता चले और उसकी उन्नति का पथ प्रशस्त होता चले। यह प्रथम भूमिका है। इसे भः क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के शिष्य को आचार्य द्वारा ‘मन्त्र दीक्षा’ दी जाती है।
मन्त्र दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि ‘‘मैं गुरु का अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा। समय समय पर उनकी सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा, अपनी सब भूलें निष्कपट रूप से उन पर प्रकट कर दिया करूंगा’’, आचार्य शिष्य को मन्त्र का अर्थ समझाता है और माता गायत्री को यज्ञोपवीत रूप से देता है। शिष्य देव भाव से आचार्य का पूजन करता है और गुरु पूजा के लिए उन्हें वस्त्र, आभूषण, पात्र, भोजन, दक्षिणा आदि की सामर्थ्यानुसार भेंट चढ़ाता है। रोली, अक्षत, तिलक, कलावा, वरण, आदि के द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे को बांधते हैं। मंत्र दीक्षा एक प्रकार से दो व्यक्तियों में आध्यात्मिक रिश्तेदारी की स्थापना है। इस दीक्षा के पश्चात् पाप पुण्य में एक प्रतिशत के भागीदार हो जाते हैं। शिष्य के सौ पापों में से एक पाप का फल गुरु को भोगना पड़ता है और गुरु के पापों का इसी प्रकार शिष्य को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पुण्य में भी एक दूसरे के साझी होते हैं। यह सामान्य दीक्षा है। यह मंत्र दीक्षा साधारण श्रेणी के सुशिक्षित सत्पुरुष, आचार्यत्व ग्रहण करके प्रारम्भिक श्रेणी के साधक को दें सकते हैं।
द्वितीय भूमिका-‘अग्नि दीक्षा’—
दूसरी भुवः भूमिका में पहुंचने पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है। इसे प्राण दीक्षा या अग्नि दीक्षा कहते हैं। प्राणमय कोश एवं मनोमय कोश के अन्तर्गत छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने की साधना का शिक्षण क्षेत्र यही है। साधन संग्राम के अस्त्र शस्त्रों को पहनना, संभालना और चलाना इसी भूमिका में सीखा जाता है। प्राण शक्ति की न्यूनता का उपचार इसी क्षेत्र में होता है। साहस, उत्साह, परिश्रम, दृढ़ता, स्फूर्ति, आशा, धैर्य, लगन, आदि वीरोचित गुणों की अभिवृद्धि इस दूसरी भूमिका में होती है। मनुष्य शरीर के अन्तर्गत ऐसे अनेक चक्र उपचक्र, भ्रमर, उपत्यय, सूत्र प्रत्यावर्तन, बीज, मेरु आदि गुप्त संस्थान होते हैं, जो प्राणमय भूमिका की साधना से जागृत होते हैं। इस जागरण के फल स्वरूप साधक में ऐसी अनेक विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसी कि साधारण मनुष्यों में नहीं देखी जातीं।
भुवः भूमिका में ही मन, बुद्धि, चित्त अहंकार के चतुष्टय का संशोधन, परिमार्जन एवं विकास होता है। यह सब कार्य ‘मध्यमा’ और ‘पश्यन्ति’ वाणी द्वारा किया जाता है। बैखरी वाणी द्वारा वचनों के माध्यम से प्रारम्भिक साधक को भूः क्षेत्र के मन्त्र दीक्षित को सलाह शिक्षा आदि दी जाती है। जब प्राण दीक्षा होती है तो गुरु अपना प्राण शिष्य के प्राण में घोल देता है। बीज रूप से अपना आत्मबल साधक के अन्तःकरण में स्थापित कर देता है। जैसे आग से आग जलाई जाती है बिजली की धारा से बल्ब जलते या पंखे चलते हैं उसी प्रकार अपना शक्ति भाग बीज रूप से दूसरे की मनोभूमि में जमा कर वहां उसे सींचा और बढ़ाया जाता है। इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं। अशक्त को सशक्त बनाना, निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराश को आशान्वित करना प्राण दीक्षा का काम है। मन्त्र से विचार उत्पन्न होता है, अग्नि से क्रिया उत्पन्न होती है। अन्तः भूमि में हलचल, क्रिया, प्रगति, चेष्टा, क्रान्ति, बेचैनी, आकांक्षा, का तीव्र गति से उदय होता है।
साधारणतया लोग आत्मोन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा देते हैं तो उसे बड़ा भारी बोझ समझते हैं, कुछ जप तप करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है मानो बहुत बड़ा मोर्चा जीत रहे हों। परन्तु जब आन्तरिक स्थिति भुवः क्षेत्र में पहुंचती है तो साधक को बड़ी बेचैनी और असंतुष्टि रहती है। उसे अपना साधन बहुत साधारण दिखाई पड़ता है और अपनी उन्नति उसे बहुत मामूली दीखती है। उसे छटपटाहट एवं जल्दी होती है कि मैं किस प्रकार शीघ्र से शीघ्र लक्ष्य तक पहुंच जाऊं? अपनी उन्नति चाहे कितने ही सुव्यवस्थित ढंग से हो रही हो पर उसे सन्तोष नहीं होता। यह व्याकुलता उसकी कोई भूल नहीं है वरन् भीतर ही भीतर जो तीव्र क्रिया शक्ति काम कर रही है, उसकी प्रतिक्रिया है। भीतरी क्रिया, प्रवृत्ति और प्रेरणा का वाह्य लक्षण असन्तोष है। यदि असन्तोष न हो तो समझना चाहिए कि साधक की क्रिया शक्ति शिथिल हो गई। जो साधक दूसरी भूमिका में है उसका असन्तोष जितना ही तीव्र होगा उतनी ही क्रिया शक्ति तेजी से काम करती रहेगी। बुद्धिमान पथप्रदर्शक, दूसरी कक्षा के साधक में सदा असन्तोष भड़काने का प्रयत्न करते हैं ताकि उसकी आन्तरिक क्रिया और भी सतेज हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह असन्तोष कहीं निराशा में परिणत न हो जाय।
अग्नि दीक्षा लेकर साधक का आन्तरिक प्रकाश स्वच्छ हो जाता है और उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अंधेरे में या धुंधले प्रकाश में बड़ी वस्तुएं भी ठीक प्रकार नहीं दीखतीं, पर तीव्र प्रकाश में मामूली चीजें भी भली प्रकार दीखती हैं और कई बार तो प्रकाश की तेजी के कारण वे वस्तुएं भी अधिक महत्वपूर्ण दीखती हैं। आत्मा में ज्ञानाग्नि का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी छोटी भूल, बुराइयां, कमियां भली प्रकार दीख पड़ती हैं। उसे मालूम पड़ता है मैं असंख्य बुराइयों का भण्डार हूं। नीची श्रेणी के मनुष्यों से भी मेरी बुराइयां अधिक है। अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार वह अपने अन्दर घृणास्पद तत्वों को बड़ी मात्रा में देखता है। जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग कतई गलती नहीं मानते उनका नीर क्षीर विवेक वह करता है। मनसा पापों तक से दुखी होता है।
महात्मा सूरदास जब परम भागवत हो रहे थे तब उन्हें अपनी बुराइयां सूझी। जब तक वे वस्तुतः पापी और व्यभिचारी रहे तब तक उन्हें अपने काम में कोई बुराई न दीखी, पर जब वे भगवान की शरण में आये तो भूतकाल की बुराइयों का स्मरण करने मात्र से उनकी आत्मा कांप गई और उनने तीव्र संवेदना को शान्त करने के लिए अपने नेत्र फोड़ डाले। फिर भी आत्म निरीक्षण करने पर उन्हें अपने भीतर दोष ही दोष दीखे, जिनकी घोषणा उन्होंने अपने प्रसिद्ध पद में की—‘‘मो सम कान कुटिल, खल, कामी’’
भुवः भूमिका में पहुंचे हुए साधक के तीन लक्षण प्रधान रूप से होते हैं (1) आत्म कल्याण के लिए तपश्चर्या में तीव्र प्रवृत्ति (2) अपनी प्रगति को मन्द अनुभव करना अपनी उन्नति के प्रति असन्तोष (3) अपने विचार, कार्य एवं स्वभाव में अनेक बुराइयों का दिखाई देना। यह भूमिका धीरे धीरे पकती रहती है। जब तक दाल नहीं पकती तब हांडी में बड़ी उथल पुथल रहती है। यदि हांडी के भीतर शान्ति हो तो उसके दो कारण समझे जा सकते हैं 1-या तो अभी पकना आरम्भ नहीं हुआ, हांडी गरम नहीं हुई 2-या पक कर दाल बिलकुल तैयार हो गई। या तो मूर्ख, अज्ञानान्धकार में डूबे हुए जड़ प्रकृति के लोग मुदित रहते हैं और अपनी बुराइयों से मौज करते हैं या फिर अन्तिम कक्षा में पहुंचा योगी आत्म साक्षात्कार करके, ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर शान्त हो जाता है। मध्यम कक्षा में तप, प्रयत्न, असंतोष एवं वेदना की प्रधानता रहती है। चूंकि यह स्थिति आवश्यक है। इसे ही आत्मा का अग्नि संस्कार कहते हैं। इसमें अन्तःकरण का परिपाक होता। शरीर को तपश्चर्याओं की अग्नि में और अन्तःकरण को असंतोष की अग्नि मं तपा कर पकाया जाता है। पूरी मात्रा मं अग्नि संस्कार हो जाने पर न तो शरीर को तपाने की आवश्यकता रहती है और न मन को तपना पड़ता है। तब वह तीसरी कक्षा ‘स्वः’ की शान्ति भूमिका है।
मन्त्र दीक्षा के लिए कोई भी विचारवान, दूरदर्शी, उच्च चरित्र, प्रतिभाशाली, सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है। वह अपनी तर्कशक्ति और बुद्धिमत्ता से शिष्य के विचारों का परिमार्जन कर सकता है। उसके कुविचारों को, भ्रमों को, सुलझाकर अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक सलाह, शिक्षण एवं उपदेश दें सकता है, अपने प्रभाव से उसे प्रभावित भी कर सकता है। अग्नि दीक्षा के लिए ऐसा गुरु चाहिए जिसके भीतर पर्याप्त मात्रा में हो, तप की पूंजी का जो धनी हो, दान वही कर सकता है जिसके पास धन हो, विद्या वही दें सकता है जिसके पास विद्या हो। जिसके पास जो वस्तु नहीं वह दूसरों को क्या देगा? जिसने स्वयं तप करके प्राण शक्ति संचित की है। अग्नि अपने भीतर प्रज्वलित कर रखी है, वही दूसरों को प्राण या अग्नि देकर उन्हें भुवः भूमिका की दीक्षा दें सकता है।
तीसरी भूमिका ब्रह्म दीक्षा—
तीसरी भूमिका ‘‘स्वः’’ है। इसे ब्रह्म दीक्षा कहते हैं। जब दूध अग्नि पर औटाकर नीचे उतार लिया जाता है और ठंडा हो जाता है तब उसमें दही का जामन देकर उसे जमा दिया जाता है, फलस्वरूप वह सारा दूध दही बन जाता है। मन्त्र द्वारा दृष्टिकोण परिमार्जन करके साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और सम्पन्नता से ओत प्रोत करता है, अग्नि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों, मलों, कषायों दुर्बलताओं को जलाता है उनसे अपना पिण्ड छुड़ाकर बन्धन मुक्त होता है एवं तप की ऊष्मा द्वारा अन्तःकरण को पका कर ब्राह्मी भूत करता है। दूध पकते पकते जब रबड़ी मलाई आदि की शकल में पहुंच जाता है तब उसका मूल्य और स्वाद बहुत बढ़ जाता है।
पहली ज्ञान भूमि दूसरी शक्ति भूमि और तीसरी ब्रह्म भूमि होती है। क्रमशः एक के बाद एक को पार करना पड़ता है। पिछली दो कक्षाओं को पा कर साधक जब तीसरी कक्षा में पहुंचता है तो उसे सद्गुरु द्वारा ब्रह्म दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। यह ‘परा’ वाणी द्वारा होती है। वैखरी वाणी द्वारा-मुंह से शब्द उच्चारण करके ज्ञान दिया जाता है। मध्यमा और पश्यन्ति वाणियों द्वारा शिष्य के प्राणमय और मनोमय कोश में अग्नि संस्कार किया जाता है। परा वाणी द्वारा-आत्मा बोलती है और उसका सन्देश दूसरी आत्मा सुनती हैं। जीभ की वाणी कान सुनते हैं, मन की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय सुनता है और आत्मा की वाणी आत्मा सुनती है। जीभ ‘वैखरी’ वाणी बोलती है। मन ‘मध्यमा’ बोलता है, हृदय की वाणी ‘पश्यन्ति’ कहलाती है और आत्मा ‘परा’ वाणी बोलती है। ब्रह्म दीक्षा में, जीभ, मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता। आत्मा के अन्तरंग क्षेत्र से जो अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है। उसे ग्रहण करने के पश्चात वह भी ऐसी ही ब्राह्मी भूत हो जाती है जैसे थोड़ा सा दही पड़ने से औटाया हुआ दूध सबका सब दही हो जाता है।
काला कोयला या सड़ी गली लकड़ी का टुकड़ा जब अग्नि में पड़ता है तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाता है और वह अग्निमय होकर अग्नि के ही सब गुणों से सुसज्जित हो जाता है। वह कोयला या लकड़ी का टुकड़ा भी अग्नि के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है और गर्मी प्रकाश तथा जलाने की शक्ति भी उसमें अग्नि के समान ही होती है। ब्राह्मी दीक्षा से ब्रह्मभूत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी अन्तरंग सत्ता ब्राह्मी भूत हो जाती है। उसे अपने भीतर बाहर चारों ओर सत् ही सत् दृष्टिगोचर होता है। विश्व में सर्वत्र उसे ब्रह्म ही ब्रह्म परिलक्षित होता।
गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया था, अर्थात् उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व के अन्तरंग में छिपी हुई अदृश्य ब्रह्म सत्ता का दर्शन कर सके। भगवान सब में व्यापक है पर उसे कोई विरले ही देखते, समझते हैं। भगवान ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी जिससे उसकी तीक्ष्ण शक्ति इतनी सूक्ष्म और पारदर्शी हो गई कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा जिसे साधारण लोक नहीं कर पाते। इस दिव्य दृष्टि को ही पाकर योगी लोग आत्मा का, ब्रह्म का, साक्षात्कार अपने भीतर और बाहर करते हैं तथा ब्राह्मी गुणों से, विचारों से स्वभावों से, कार्यों से, ओत प्रोत हो जाते हैं। यशोदा ने, कौशल्या ने, काकभुषुण्डि ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि पाई थी और ब्रह्म का साक्षात्कार किया था, ईश्वर का दर्शन इसे ही कहते हैं। ब्रह्म दीक्षा पाने वाले शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और स्थिति वैसे ही अनुभव करता है जैसे कोयला अग्नि में पड़कर अपने को अग्निमय अनुभव करता है।
द्विजत्व की तीन कक्षाएं हैं (1) ब्राह्मण (2) क्षत्रिय (3) वैश्य। पहली कक्षा है—वैश्य। वैश्य का उद्देश्य है, सुख सामग्रियों का उपार्जन। मन्त्र (विचार) द्वारा वह लोग व्यवहार सिखाया जाता है, वह दृष्टिकोण दिया जाता है जिसके द्वारा सांसारिक जीवन सुखमय, शान्तिपूर्ण, सफल एवं सुसम्पन्न बन सके। बुरे गुण, कर्म, स्वभावों के कारण लोग अपने आपको चिन्ता, भय, दुःख, रोग, क्लेश, एवं दरिद्रता के चंगुल में फंसा लेते हैं यदि उनका दृष्टिकोण सही हो, दश शूलों से बचे रहें तो निश्चय ही मानव जीवन स्वर्गीय आनन्द से ओत प्रोत होना चाहिए।
क्षत्रिय तत्व का आधार है शक्ति। शक्ति तप से उत्पन्न होती है। दो वस्तुओं को घिसने में गर्मी पैदा होती है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। बिजली की उत्पत्ति घर्षण से होती है। बुराइयों के, त्रुटियों के, कुसंस्कारों के विकारों के विरुद्ध संघर्ष कार्य को तप कहते हैं। तप से आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है और उसे जिस दिशा में भी प्रयुक्त किया जाय उसी में चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। शक्ति स्वयं ही चमत्कार है। शक्ति का नाम ही सिद्धि है। अग्नि दीक्षा से तप का प्रारम्भ होता है, आत्म दमन के लिए युद्ध छेड़ा जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि तू ‘‘निरन्तर युद्ध कर’’ निरन्तर युद्ध किससे करता? महाभारत तो थोड़े ही दिन में समाप्त हो गया था, फिर अर्जुन निरन्तर किससे लड़ता? भगवान का संकेत आन्तरिक शत्रुओं से संघर्ष जारी रखने का था। यही अग्नि दीक्षा का उपदेश था। अग्नि दीक्षा से दीक्षित के क्षत्रियत्व का, साहस का, शौर्य का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का विकास होता है। इससे यह यश का भागी बनता है।
मन्त्र दीक्षा से साधक व्यवहार कुशल बनता है और अपने जीवन को सुख, शान्ति, सहयोग एवं सम्पन्नता से भरा पूरा कर लेता है। अग्नि दीक्षा से उसकी प्रतिमा प्रतिष्ठा ख्याति, प्रशंसा एवं महानता का प्रकाश होता है। दूसरों का सिर उसके चरणों पर स्वतः झुक जाता है। लोग उसे नेता मानते हैं उसका अनुसरण और अनुगमन करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त दो दीक्षाओं द्वारा वैश्व और क्षत्रिय बनने के उपरान्त साधक ब्राह्मण बनने के लिए अग्रसर होता है। ब्रह्म दीक्षा से उसे ‘‘दिव्य दृष्टि’’ मिलती है। इसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं।
शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। अर्जुन को भगवान ने ‘‘दिव्यं ददामि ते चक्षुम्’’ दिव्य नेत्र देकर अपने विराट् स्वरूप का दर्शन सम्भव करा दिया था। यह तृतीय नेत्र हर योगी का खुलता है, उसे वे बातें दिखाई पड़ती हैं जो साधारण व्यक्तियों को नहीं दीखतीं। उनको कण कण में परमात्मा का पुण्य प्रकाश बहुमूल्य रत्नों की तरह जगमगाता हुआ दिखाई देता है। भक्त माइकेल को प्रत्येक शिला में एक स्वर्गीय अप्सरा दिखाई पड़ती थी। सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि बड़ी संकुचित होती है वे आज के हानि लाभों में ही रोते हंसते हैं पर ब्रह्मज्ञानी दूर तक देखता है, वह वस्तु स्थिति पर पारदर्शी विचार करता है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की लीला एवं दया का अनुभव करता हुआ प्रसन्न रहता है। विश्व मानव की सेवा में ही वह अपना जीवन लगाता है। इस प्रकार ब्रह्म दीक्षा में दीक्षित हुआ साधक परम भागवत होकर, परम शान्ति को अन्तःकरण में धारण करता हुआ दिव्य तत्वों से परिपूर्ण होता जाता है। इस श्रेणी के साधकों को ही भूसुर कहते हैं।
कल्याण मन्दिर प्रवेश द्वार :—
तीन दीक्षाओं से तीन वर्णों में प्रवेश मिलता है। दीक्षा का अर्थ है—विधिवत् व्यवस्थित कार्यक्रम और निश्चित श्रद्धा। यों कोई विद्यार्थी नियत कोर्स न पढ़कर, नित्य कक्षा में न बैठ कर, कभी कोई, कभी कोई, पुस्तक पढ़ता रहे तो भी धीरे उसका ज्ञान बढ़ता ही रहेगा और क्रमशः उसके ज्ञान में उन्नति होती ही जायगी। सम्भव है वह अव्यवस्थित क्रम से भी ग्रेजुएट बन जाय, पर यह मार्ग है कष्ट साध्य और लम्बा। क्रमशः एक एक कक्षा पार करते हुए एक एक कोर्स पूरा करते हुए, निर्धारित क्रम से यदि पढ़ाई जारी रखी जाय तो अध्यापक को भी सुविधा रहती है और विद्यार्थी को भी। यदि विद्यार्थी आज कक्षा 5 की कल कक्षा 10 की, आज संगीत की, कल डाक्टरी की, पुस्तकें पढ़े तो उसे याद करने में और शिक्षक को पढ़ाने में असुविधा होगी। इसलिए ऋषियों ने आत्मोन्नति की तीन भूमिकाएं निर्धारित करदी हैं। द्विजत्व को तीन भागों में बांट दिया है। क्रमशः एक एक कक्षा में प्रवेश करना और नियम, प्रतिबन्ध, आदेश एवं अनुशासन को श्रद्धा पूर्वक मानना इसी का नाम दीक्षा है।
तीन कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए तीन बार भर्ती होना पड़ता है। कई जगह एक ही अध्यापक तीनों कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कई जगह हर कक्षा के लिए अलग अध्यापक होते हैं कई बार तो स्कूल ही बदलने पड़ते हैं। प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करके हाईस्कूल में भर्ती होना पड़ता है। और हाई स्कूल पास करके कालेज में नाम लिखाना पड़ता है। तीनों विद्यालयों की पढ़ाई पूरी करने पर एम.ए. की पूर्णता प्राप्त होती है।
इन तीन कक्षाओं के अध्यापकों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। प्रथम कक्षा में सद् विचार और सत् आचार सिखाया जाता है। इसके लिए कथा, प्रवचन, सत्संग, भाषण, पुस्तक, प्रचार, शिक्षण, सलाह, तर्क आदि साधन काम में लाये जाते हैं। इनके द्वारा मनुष्य की विचार भूमिका का सुधार होता है, कुविचारों के स्थान पर सद्विचार स्थापित होते हैं, जिनके कारण साधक अनेक शूलों और क्लेशों से बचता हुआ, सुख शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत कर लेता है। इस प्रथम कक्षा के विद्यार्थी को गुरु के प्रति ‘श्रद्धा’ रखना आवश्यक है। श्रद्धा न होगी तो उन वचनों का, उपदेशों का न तो महत्व समझ में आवेगा और न उन पर विश्वास होगा। प्रत्यक्ष है कि उसी बात को कोई महापुरुष कहे तो लोग उसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी बात को यदि तुच्छ मनुष्य कहे तो कोई कान नहीं देता। दोनों ने एक ही बात कही पर एक के कहने पर उपेक्षा की गई दूसरे के कहने पर ध्यान दिया गया इसमें कहने वाले के ऊपर सुनने वालों की श्रद्धा या अश्रद्धा का होना ही प्रधान कारण है। किसी व्यक्ति पर विशेष श्रद्धा हो तो उसकी साधारण बातें भी असाधारण प्रतीत होती हैं।
रोज सैकड़ों कथा, प्रवचन, व्याख्यान होते हैं। अखबारों में, पर्चों, पोस्टरों में तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं, रेडियो से नित्य ही उपदेश सुनाएं जाते हैं पर उन पर कोई कान नहीं देता, कारण यही है सुनने वाले की उन सुनाने वालों के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं होती, इसलिए वे महत्वपूर्ण बातें भी निरर्थक एवं उपेक्षणीय मालूम देती हैं। कोई उपदेश तभी प्रभावशाली हो सकता है जब उसका देने वाला, सुनने वालों का श्रद्धास्पद हो। वह श्रद्धा जितनी ही तीव्र होगी उतना ही अधिक उपदेश का प्रभाव पड़ेगा। प्रथम कक्षा के मन्त्र दीक्षित गायत्री का समुचित लाभ उठा सकें इस दृष्टि से साधक को, दीक्षित को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखेगा। उसे वह देवतुल्य या परमात्मा का प्रतीक मानेगा। इसमें कुछ विचित्रता भी नहीं है। श्रद्धा के कारण जब मिट्टी पत्थर और धातु की बनी मूर्तियां, हमारे लिए देव बन जाती हैं तो कोई कारण नहीं कि एक जीवित मनुष्य में देवत्व का आरोपण करके अपनी श्रद्धानुसार अपने लिए उसे देव न बना लिया जाय।
श्रद्धा का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता :—
एकलव्य भील ने, मिट्टी के द्रोणाचार्य बना कर उनसे बाण विद्या सीखी थी, और उस मूर्ति ने उस भील को बाण विद्या का इतना पारंगत कर दिया था कि उसके द्वारा वाणों से कुत्ते का मुंह सी दिये जाने पर द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष पढ़ने वाले पाण्डवों को ईर्ष्या हुई थी। स्वामी रामानन्द के मना करते रहने पर भी कबीर उनके शिष्य बन बैठे और अपनी तीव्र श्रद्धा के कारण वह लाभ प्राप्त किया जो उनके विधिवत् दीक्षित शिष्यों में से एक भी प्राप्त न कर सका था। रजोधर्म होने पर गर्भाशय में एक बूंद वीर्य का पहुंच जाना गर्भ धारण कर देता है। जिसे रजो दर्शन न होता हो उस बन्ध्या स्त्री के लिए पूर्ण पुंसत्व शक्ति वाला पति भी गर्भ स्थापित नहीं करा सकता। श्रद्धा एक प्रकार का रजोधर्म है, जिससे साधक के अन्तःकरण में सदुपदेश जमते और फलते फूलते हैं। अश्रद्धालु के मन पर ब्रह्मा का उपदेश भी कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता। श्रद्धा के अभाव में किसी महापुरुष के दिन रात साथ रहने पर भी कोई व्यक्ति कुछ लाभ नहीं उठा सकता है और श्रद्धा होने पर दूरस्थ व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है। इसलिए आरम्भिक कक्षा के मन्त्र दीक्षित को गुरु के प्रति तीव्र श्रद्धा की धारणा करनी पड़ती है।
विचारों को मूर्तिमान रूप देने के लिए उनको प्रकट रूप से व्यवहार में लाना पड़ता है। जितने भी धार्मिक कर्म-काण्ड, दान-पुण्य, व्रत-उपवास, हवन-पूजन, कथा-कीर्तन आदि हैं वे सब इसी प्रयोजन के लिए हैं कि आन्तरिक श्रद्धा व्यवहार में प्रकट होकर साधक के मन में परिपुष्ट हो जाय। गुरु के प्रति मन्त्र दीक्षा में ‘‘श्रद्धा’’ की शर्त होती है। श्रद्धा न हो या शिथिल हो तो वह दीक्षा केवल चिन्ह पूजा मात्र है। अश्रद्धालु की गुरु दीक्षा से कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। दीक्षा के समय स्थापित हुई श्रद्धा, कर्मकाण्ड के द्वारा सजग रहे इसी प्रयोजन के लिए समय समय पर गुरु पूजन किया जाता है। दीक्षा के समय वस्त्र, पात्र, पुष्प भोजन, दक्षिणा द्वारा गुरु का पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ सुदी 15) को यथा शक्ति उनके चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में कुछ भेंट पूजा अर्पित करते हैं। यह प्रथा अपनी आन्तरिक श्रद्धा को मूर्त रूप देने, बढ़ाने एवं परिपुष्ट करने के लिए है। केवल विचार मात्र से कोई भावना परिपक्व नहीं होती। क्रिया और विचार दोनों के सम्मिश्रण से एक संस्कार बनता है, जो मनोभूमि में स्थिर होकर आशा जनक परिणाम उपस्थित करता है।
प्राचीन काल में यह नियम था कि गुरु के पास जाने पर शिष्य कुछ वस्तु भेंट के लिए ले जाता था चाहे वह कितने ही स्वल्प मूल्य की क्यों न हो। समिधा की लकड़ी हाथ में लेकर शिष्य गुरु के सम्मुख जाते थे इसे ‘समित्पाणि’ कहते थे। वे समिधाएं उनकी श्रद्धा की प्रतीक होती हैं चाहे उनका मूल्य कितना ही कम क्यों न हो। शुकदेव जी जब राजा जनक के पास ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने गये तो राजा जनक मौन रहे उनने एक शब्द भी उपदेश न दिया। शुकदेव जी वापिस लौट आये। पीछे उन्हें ध्यान आया कि भले ही मैं संन्यासी हूं, राजा जनक, गृहस्थ हैं, पर जब कि मैं उनसे कुछ सीखने गया तो अपनी श्रद्धा का प्रतीक साथ लेकर जाना चाहिए था। दूसरी बार शुकदेव जी हाथ में समिधाएं लेकर नम्र भाव से उपस्थित हुए तो उनने विस्तार पूर्वक ब्रह्म विद्या समझाई।
श्रद्धा न हो तो सुनने वाले का और कहने वाले का श्रम तथा समय निरर्थक जाता है। इसलिए शिक्षण के समान ही श्रद्धा बढ़ाने का भी प्रयत्न जारी रहना चाहिए। निर्धन व्यक्ति भले ही न्यूनतम मूल्य की वस्तुएं ही क्यों भेट न करें उन्हें सदैव गुरु को बार बार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भेट पूजन एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे श्रद्धा रूपी ‘‘ग्रहण शक्ति’’ का तीव्र विकास होता है। श्रद्धा ही वह अस्त्र है जिससे परमात्मा को पकड़ा जा सकता है। भगवान और किसी वस्तु से वश में नहीं आते वे केवल मात्र श्रद्धा के ब्रह्म पास में ही फंस कर भक्त के गुलाम बनते हैं। ईश्वर को परास्त करने का एटम बम श्रद्धा ही है। इस महानतम दैवी सम्मोहनास्त्र को बनाने और चलाने का प्रारम्भिक अभ्यास गुरु से किया जाता जब यह शस्त्र भली प्रकार हाथ में आ जाता है तो उससे भगवान को वश में कर लेना साधक के बाएं हाथ का खेल हो जाता है।
आरम्भिक कक्षा का रसास्वादन करने पर साधक की मनोभूमि काफी सुदृढ़ और परिपक्व हो जाती है। वह भौतिकवाद की तुच्छता और आत्मिकवाद की महानता व्यवहारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से दार्शनिक दृष्टि से समझ लेता है, तब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा लाभ आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने में ही है। श्रद्धा परिपक्व होकर जब निष्ठा के रूप में परिणित हो जाती है तो वह भीतर से काफी मजबूत हो जाती है। अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए उसमें इतनी दृढ़ता होती है कि वह कष्ट सह सके तप कर सके, त्याग की परीक्षा का अवसर आवे तो विचलित न हो। जब ऐसी पक्की मनोभूमि होती है जो ‘गुरु’ द्वारा उसे अग्नि दीक्षा देकर कुछ और गरम किया जाता है जिससे उसके मल जल जायं, कीर्ति का प्रकाश हो तथा तप की अग्नि में पक कर वह पूर्णता को प्राप्त हो।
तपस्वी की गुरु दक्षिणा :—
गीली लकड़ी को केवल धूप में सुखाया जाता है। उसे थोड़ी सी गर्मी पहुंचाई जाती है। धीरे धीरे उसकी नमी सुखाई जाती है। पर जब वह भली प्रकार सूख जाती है तो उसे अग्नि में देकर मामूली लकड़ी से महा शक्तिशाली प्रचंड अग्नि के रूप में परिणित कर दिया जाता है। गीली लकड़ी को चूल्हे में दिया जाय तो उसका परिणाम अच्छा न होगा। प्रथम कक्षा के साधक पर केवल गुरु श्रद्धा की जिम्मेदारी है और दृष्टिकोण को सुधार कर अपना प्रत्यक्ष जीवन सुधारना होता है। यह सब प्रारम्भिक छात्र के उपयुक्त है। यदि आरम्भ में ही तीव्र साधना में नये साधक को फंसा दिया जाय तो वह बुझ जायगा। तप की कठिनाई देखकर वह डर जायगा और प्रयत्न छोड़ बैठेगा। दूसरी कक्षा का छात्र चूंकि धूप में सूख चुका है इसलिए उसे कोई विशेष कठिनाई मालूम नहीं देती वह हंसते हंसते साधना के श्रम का बोझ उठा लेता है।
अग्नि दीक्षा के साधक को तपाने के लिए कई प्रकार के संयम, व्रत, नियम, त्याग आदि करने कराने होते हैं। प्राचीन काल में उद्दालक, धौम्य, आरुणि, उपमन्यु, कच, श्लीमुख, जरुत्कार, हरिश्चन्द्र, दशरथ, नचिकेता, शेष, विरोचन, जाबालि सुमनस, अम्बरीष, दलीप आदि अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं के आदेशानुसार अनेक कष्ट सहे और उनके बताये हुए कार्यों को पूरा किया। स्थूल दृष्टि से इन महापुरुषों के साथ गुरुओं को जो व्यवहार था वह ‘हृदय हीनता’ कहा जा सकता है। पर सच्ची बात यह है कि उन्होंने स्वयं निन्दा और बुराई को अपने ऊपर ओढ़ कर शिष्यों को अनन्त काल के लिए प्रकाशवान एवं अमर कर दिया। यदि कठिनाइयों में होकर राजा हरिश्चन्द्र को न गुजरना पड़ा होता तो वे भी असंख्यों राजा रईसों की भांति विस्मृति के गर्त में चले गये होते।
अग्नि दीक्षा पाकर शिष्य गुरू से पूछता है कि—‘‘आदेश कीजिए, कि मैं आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा उपस्थित करूं?’’ गुरू देखता है कि शिष्य की मनोभूमि, सामर्थ्य, योग्यता, श्रद्धा, त्याग वृत्ति कितनी है उसी आधार पर वह उससे गुरू दक्षिणा मांगता है। यह याचना अपने लिए रुपया पैसा, धन दौलत देने के रूप में कदापि नहीं हो सकती। सद्गुरु सदा परम त्यागी, अपरिग्रही, कष्ट सहिष्णु एवं स्वल्प संतोषी होते हैं। उन्हें अपने लिए शिष्य से या किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जो गुरु अपने लिए कुछ मांगता है वह गुरु नहीं भिक्षुक है। ऐसे लोग गुरु जैसे परम पवित्र पद के अधिकारी कदापि नहीं हो सकते। अग्नि दीक्षा देकर गुरु जो कुछ मांगता है वह शिष्य को अधिक उज्ज्वल, अधिक सुदृढ़, अधिक उदार, अधिक तपस्वी, बनाने के लिए होता है। यह याचना उसके यश का विस्तार करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए, एवं उसे त्याग का आत्म संतोष देने करने के लिए होती है।
‘‘गुरु दक्षिणा मांगिए’’ शब्दों में शिष्य कहता है कि ‘मैं सुदृढ़ हूं, मेरी आत्मिक स्थिति की परीक्षा लीजिए।’ स्कूल कालेजों में परीक्षा ली जाती है। उत्तीर्ण छात्र की योग्यता एवं प्रतिष्ठा को, वह उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र अनेक गुना बढ़ा देता है। परीक्षा न दी जाय तो योग्यता का क्या पता चले? संसार में किसी व्यक्ति की महानता का पुण्य प्रसार करने के लिए, उसके गौरव को सर्व साधारण पर प्रकट करने के लिए, साधक को अपनी महानता पर आत्म विश्वास कराने के लिए, गुरु अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगता है। शिष्य उसे देकर धन्य हो जाता है।
प्रारम्भिक कक्षा में मंत्र दीक्षा का शिष्य सामर्थ्यानुसार गुरु पूजन करता है। श्रद्धा रखना और उसकी सलाहों के अपने दृष्टिकोण को सुधारना, बस इतना ही उसका कार्य क्षेत्र है। न वह गुरु दक्षिणा मांगने के लिए गुरु से कहता है और न गुरु उससे मांगता ही है। दूसरी कक्षा का शिष्य अग्नि दीक्षा लेकर ‘‘गुरु दक्षिणा मांगने’’ के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करता है। गुरु इस कृपा को करना स्वीकार कर के शिष्य की प्रतिष्ठा महानता, कीर्ति एवं प्रमाणिकता में चार चांद लगा देता है गुरु की याचना सदैव ऐसी होती है जो सबके लिए, सब दृष्टियों से, परम कल्याण कारक हो, उस व्यक्ति का तथा समाज का उससे भला होता हो। कई बार निर्बल मनोभूमि को लोग भी आगे बढ़ाये जाते हैं उनसे गुरु दक्षिणा में ऐसी छोटी चीज मांगी जाती है जिन्हें सुनकर हंसी आती है। अमुक फल, अमुक शाक, अमुक मिठाई आदि का त्याग कर देने जैसी याचना कुछ महत्व नहीं रखती। पर शिष्य का मन हलका हो जाता है वह अनुभव करता है कि मैंने त्याग किया, गुरु के आदेश का पालन किया गुरु दक्षिणा चुका दी, ऋण से उऋण हो गया और परीक्षा उत्तीर्ण करली। बुद्धिमान गुरु साधक की मनोभूमि और आन्तरिक स्थिति देखकर ही उसे तपाते हैं।
ब्रह्म दीक्षा की दक्षिणा ‘आत्म दान’ :—
क्रमशः दीक्षा का महत्व बढ़ता है, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ता है। जो वस्तु जितनी बढ़िया होती है उसका मूल्य भी उसी अनुपात से होता है। लोहा सस्ता बिकता है। कम पैसे देकर मामूली दुकानदार से लोहे की वस्तु खरीदी जा सकती है पर यदि सोना या जवाहरात खरीदने हों तो ऊंची दुकान जाना पड़ेगा और बहुत दाम खर्च करना पड़ेगा। ब्रह्म दीक्षा में न विचार शक्ति से काम चलता है और न प्राण शक्ति से। एक आत्मा दूसरी आत्मा से ‘परा’ वाणी द्वारा वार्तालाप करती हैं। आत्मा की भाषा को ‘परा’ कहते हैं। वेखरी वाणी को कान सुनते हैं, ‘मध्यमा’ को मन सुनता है, पश्यन्ति हृदय को सुनाई पड़ती है और ‘परा’ वाणी द्वारा दो आत्माओं में संभाषण होता है। अन्य वाणियों की बात आत्मा नहीं पाती। जैसे चींटी की समझ में मनुष्य की वाणी नहीं आती और मनुष्य चींटी की वाणी को नहीं सुन पाता, उसी प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नहीं पहुंचते उपनिषद् का वचन है कि ‘‘बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्त नहीं होती। बल हीनों को भी वह प्राप्त नहीं होती’’ कारण स्पष्ट है यह बातें आत्मा तक पहुंचती ही नहीं तो वह सुनी कैसे जायगी!
कीचड़ में फंसे हुए हाथी को दूसरा हाथी ही निकालता है। पानी में बहते जाने वाले को कोई तैरने वाला ही पार निकालता है। राजा की सहायता करना किसी राजा को ही सम्भव है। एक आत्मा में ब्रह्म ज्ञान जागृत करना, उसे ब्राह्मीभूत, ब्रह्म परायण बनाना केवल उसी के लिए संभव है जो स्वयं ब्रह्म तत्व से ओत प्रोत हो रहा हो। जिसमें स्वयं अग्नि होगी वही दूसरों को प्रकाश और गर्मी दे सकेगा अन्यथा अग्नि का चित्र कितना ही आकर्षक क्यों न हो उससे कुछ पकाने का प्रयोजन सिद्ध न होगा।
कई व्यक्ति साधु महात्माओं का भेष बना लेते हैं पर उनमें ब्रह्मतेज की अग्नि नहीं होती, जिसमें साधुता हो वही साधु है, जिसकी आत्मा महान् हो वही महात्मा है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण है, जिसने रागों से मन को बचा लिया है वही वैरागी है, जो स्वाध्याय में मनन में लीन रहता हो वही मुनि है, जिसने अहंकार को मोह ममता को त्याग दिया है वही संन्यासी है, जो तप में प्रवृत्त हो वही तपसी है। कौन क्या है? इसका निर्णय गुण कर्म से होता है, वेश से नहीं। इसलिए ब्रह्म परायण होने के लिए कोई वेश से नहीं। इसलिए ब्रह्म परायण होने के लिए कोई वेश बनाने की आवश्यकता नहीं। दूसरों को बिना प्रदर्शन किये, सीधे साधे तरीके से रहकर जब आत्म कल्याण किया जा सकता है तो व्यर्थ में लोक दिखावा क्यों किया जाय? सादा वस्त्र, सादा वेष और सादा जीवन में जब महानतम आत्मिक साधना हो सकती है तो असाधारण वेश तथा अस्थिर कार्यक्रम क्यों अपनाया जाय? पुराने समय अब नहीं रहे, पुरानी परिस्थितियां भी अब नहीं है। आज की स्थिति में सादा जीवन में ही आत्मिक विकास की संभावना अधिक है।
ब्राह्मी दृष्टि का, दिव्य दृष्टि का, प्राप्त होना ही ब्रह्म समाधि है। सर्वत्र सब में ईश्वर का दिखाई देना, अपने अन्दर तेज पुंज की उज्ज्वल झांकी होना, अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य, दैवी हो जाना, यही ब्राह्मी स्थिति है। पूर्व युगों में आकाश तत्व की प्रधानता थी दीर्घ काल तक प्राणों को रोक कर ब्रह्माण्ड में एकत्रित कर लेना और शरीर को निःचेष्ट कर देना ‘समाधि’ कहलाता था उन युगों में वायु और अग्नि तत्वों की प्रधानता थी। आज के युग में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से ब्राह्मी स्थिति को ही समाधि कहते हैं। इस युग के सर्व श्रेष्ठ शास्त्र ‘भगवद् गीता’ के दूसरे अध्याय में इसी ब्रह्म समाधि की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी गई है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्म समाधिस्थ ही कहा जायगा।
अब भी कई व्यक्ति जमीन में गड्ढे खोद कर उनमें बन्द हो जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं। यह बाल क्रीड़ा अत्यन्त उपहासास्पद है। वह मन की घबराहट पर काबू पाने की मानसिक साधना का चमत्कार मात्र है। अन्यथा लम्बे चौड़े गड्ढे में कोई भी आदमी काफी लम्बी अवधि तक सुख पूर्वक रह सकता है। रात भर लोग रुई की रजाई में मुंह बन्द करके सोते रहते हैं रजाई के भीतर की जरा सी हवा से रात भर का गुजारा हो जाता है तो लम्बे चौड़े गड्ढे की हवा आसानी से दस पन्द्रह दिन काम दे सकती है। फिर भूमि में स्वयं भी हवा रहती है। गुफाओं में रहने का अभ्यासी मनुष्य आसानी से जमीन में गढ़ने की समाधि का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे क्रीड़ा कौतुकों की ओर ध्यान देने की सच्चे ब्रह्मज्ञानी को कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती।
परावाणी द्वारा अन्तरंग प्रेरणा
आत्मा में ब्रह्म तत्व का प्रवेश करने में दूसरी आत्मा द्वारा आया हुआ ब्रह्म संस्कार बड़ा काम करता है। सांप जब किसी को काटता है तो तिल भर जगह में दांत गढ़ता है, और विष भी कुछ रत्ती ही डालता है। पर वह तिल भर जगह में डाला हुआ रत्ती भर विष धीरे धीरे सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है, सारी देह विषैली हो जाती है और अन्त में परिणाम मृत्यु होता है। ब्रह्म दीक्षा भी आध्यात्मिक ‘सर्प दंशन’ है। एक का विष दूसरे को चढ़ जाता है। अग्नि की एक चिनगारी सारे ढेर को अग्नि रूप कर देती है। भले प्रकार स्थिति किया हुआ दीक्षा संस्कार, तेजी से फैलती है थोड़े ही समय में पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और आध्यात्मिक प्रवचन सुनते रहने से मनोभूमि तो तैयार होती है पर बीज बोये बिना अंकुर नहीं उगता, और अंकुर को सींचे बिना, शीतल छाया और मधुर फल देने वाला वृक्ष नहीं होता। स्वाध्याय और सत्संग के अतिरिक्त आत्म कल्याण के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है। साधना की जड़ में सजीव प्राण और सजीव प्रेरणा हो तो वह अधिक सुगमता और सुविधा पूर्वक विकसित होती है।
ब्राह्मी स्थिति का साधक, अपने भीतर और बाहर ब्रह्म का पुण्य प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह ब्रह्म की गोदी में किलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिन्धु में आनन्द मग्न हो रहा है। इस दशा में पहुंच कर वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो प्रारब्ध बन चुके हैं उन कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए वह जीवित रहता है। जब वह हिसाब बराबर हो जाता है तो पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण ब्राह्मी स्थिति में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर उसे भव बन्धन में लौटना नहीं होता। प्रारब्धों को पूरा करने के लिए वह शरीर धारण किये रहता है, सामान्य श्रेणी के मनुष्यों की भांति सीधा साधा जीवन बिताता है, तो भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची होती है। हमारी जानकारी में ऐसे अनेक ऋषि राजर्षि और ब्रह्मर्षि हैं जो बाह्यतः बहुत ही साधारण रीति से जीवन बिता रहे हैं पर उनकी आन्तरिक स्थिति सतयुग आदि के श्रेष्ठ ऋषियों के समान ही महान है। युग प्रभाव से आज चमत्कारों का युग नहीं रहा तो भी आत्मा की उन्नति में कभी कोई युग बाधा नहीं डाल सकता। पूर्व काल में जैसी महान आत्माएं होती थीं, आज भी वह सब क्रम यथावत जारी है। उस समय वे योगी आसानी से पहचान लिये जाते थे, आज उनका पहचानना कठिन है। इस कठिनाई के होते हुए भी आत्म विकास का मार्ग सदा की भांति अब भी खुला हुआ है।
ब्रह्म दीक्षा के अधिकारी गुरु शिष्य ही इस महान सम्बन्ध को स्थापित कर सकते हैं। शिष्य, गुरु को आत्म समर्पण करता है, गुरु उसके कार्यों का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपने ऊपर लेता है। ईश्वर को आत्म समर्पण करने की प्रथम भूमिका गुरु को आत्म समर्पण करना है। शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समर्पण करता है। गुरु उस सबको अमानत के तौर पर शिष्य को लौटा देता है और आदेश कर देता है कि इन सब वस्तुओं को गुरु की समझ कर उपयोग करो इस समर्पण से प्रत्यक्षतः कोई विशेष हेर फेर नहीं होता। क्यों कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु अपरिग्रही होने के कारण उस सब ‘समर्पण’ का करेगा भी क्या? दूसरे व्यवस्था एवं व्यवहारिकता की दृष्टि से भी उसका सौंपा हुआ सब कुछ उसी के संरक्षण में ठीक प्रकार रह सकता है। इसलिए बाह्यतः इस समर्पण में कुछ विशेष बात प्रतीत नहीं होती पर आत्मिक दृष्टि से इस ‘आत्म दान’ का मूल्य इतना भारी है कि उसकी तुलना और किसी त्याग या पुण्य से नहीं हो सकती।
जब दो चार रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्म संतोष और पुण्य प्राप्त होता है तब शरीर भी दान कर देने से पुण्य और आत्म संतोष की अन्तिम मर्यादा समाप्त हो जाती है। आत्म दान से बड़ा और कोई दान इस संसार में किसी प्राणी से सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए इसकी तुलना में इस विश्व ब्रह्माण्ड में और कोई पुण्य फल भी नहीं है। नित्य सवा मन सोने का दान करने वाला कर्ण ‘दान वीर’ के नाम से प्रसिद्ध था, पर उसके पास भी दान के बाद कुछ न कुछ अपना रह जाता था। जिस दानी ने अपना कुछ छोड़ा ही नहीं उसकी तुलना किसी दानी से नहीं हो सकती।
‘आत्म दान’ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महान कार्य है। अपनी सब वस्तुएं जब वह गुरु की, अन्त में परमात्मा की, समझ कर उनके आदेशानुसार नौकर की भांति प्रयोग करता है, तो उसके स्वार्थ, मोह, अहंकार, मान, मद, मत्सर, क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं। जब अपना कुछ रहा ही नहीं तो ‘मेरा’ क्या? अहंकार किस बात का? जब उपार्जित की हुई वस्तुओं का स्वामी गुरु या परमात्मा ही है तो स्वार्थ कैसा? जब हम नौकर मात्र रह गये तो हानि लाभ में शोक संताप कैसा? इस प्रकार ‘आत्म दान’ में वस्तुतः ‘अहंकार’ का दान होता है। वस्तुओं के प्रति ‘मेरी’ भावना न रहकर ‘गुरु की’ या परमात्मा की भावना हो जाती है। यह ‘‘भावना परिवर्तन’’ आत्म परिवर्तन-एक असाधारण एवं रहस्यमय प्रक्रिया है। इसके द्वारा साधक सहज ही बन्धनों से खुल जाता है। अहंकार के कारण जो अनेक संस्कार उसके ऊपर लदते थे वे एक भी उसके ऊपर नहीं लदते। जैसे छोटा बालक अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता, उसका सब कुछ बोझ माता पिता पर रहता है। इसी प्रकार आत्म दानी का बोझ भी किसी दूसरी उच्च सत्ता पर चला जाता है।
ब्रह्म दीक्षा का शिष्य गुरु को ‘आत्म दान’ करता है। मंत्र दीक्षित को ‘गुरु पूजा’ करनी पड़ती है। अग्नि दीक्षित को ‘गुरु दीक्षा’ देनी पड़ती है। ब्रह्म दीक्षित को आत्म समर्पण करना पड़ता है। राम को राज्य का अधिकारी मानकर उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर रख कर जैसे भरत राज काज चलाते रहे वैसे ही आत्म दानी अपनी वस्तुओं का समर्पण करके उनके व्यवस्थापक के रूप में स्वयं काम करता रहता है।
वर्तमानकालीन कठिनाइयाँ - आत्मकल्याण की तीन कक्षाएँ -
गायत्री द्वारा आत्म विकास की तीनों कक्षाएं पार की जाती हैं। सर्व साधारण की जानकारी के लिए ‘‘गायत्री महाविज्ञान’’ के तीन खंडों में यथा सम्भव उपयोगी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। उन पुस्तकों में वह शिक्षा मौजूद है जिसे दृष्टिकोण का परिमार्जन एवं मंत्र दीक्षा कहते हैं। यज्ञोपवीत का रहस्य, गायत्री ही कल्प वृक्ष है, गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री रामायण, गायत्री उपनिषद्, गायत्री की दस भुजा आदि प्रकरणों में यह बताया गया है। कि हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में संशोधन करके किस प्रकार सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं तीनों खंडों में अग्नि दीक्षा की द्वितीय भूमिका की शिक्षा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। ब्रह्म संध्या, अनुष्ठान, ध्यान पाप नाशक तपश्चर्याएं, उद्यापन विशेष साधनाएं, उपवास, प्राण विद्या, मनोमय कोश की साधना, तंत्र, पुरश्चरण आदि प्रकरणों में शक्ति उत्पन्न करने की शिक्षा दी गई है। ब्रह्म दीक्षा की शिक्षा गायत्री पंजर, गायत्री हृदय, कुंडलिनी जागरण, ग्रन्थि भेद, विज्ञानमय कोश की वेधना एवं आनन्दमय कोश की साधना के अन्तर्गत भली प्रकार दी गई है। शिक्षाएं इस प्रकार मौजूद ही हैं उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करने से कई बार दुष्प्राप्य वस्तुएं भी मिल जाती हैं।
यदि उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो किसी स्वर्गीय, पूर्व कालीन या दूरस्थ व्यक्ति की प्रतिमा को गुरु मानकर यात्रा आरम्भ की जा सकती है। आवश्यक परम्परा का लोप न हो जाय इसलिए किसी साधारण श्रेणी के सत्पात्र से भी काम चलाया जा सकता है। गुरु का निर्लोभ, निरहंकारी एवं शुद्ध चरित्र होना आवश्यक है। यह योग्यताएं जिस व्यक्ति में हों, वह काम चलाऊ गुरु के रूप में काम दें सकता है। यदि उसमें शक्ति दान एवं पथ प्रदर्शक की योग्यता न होगी तो भी वह अपनी श्रद्धा को बढ़ाने में साथी की तरह सहयोग अवश्य देगा। ‘निगुरा’ रहने की अपेक्षा मध्यम श्रेणी के पथ प्रदर्शक से काम चल सकता है। गेहूं न मिले तो ज्वार बाजरा खाकर भी काम चलता है। यज्ञोपवीत धारण करने एवं गुरु दीक्षा लेने की प्रत्येक द्विज को अनिवार्य आवश्यकता है। चिह्न पूजा के रूप में यह प्रथा चलती रहे तो समयानुसार उसमें सुधार भी हो सकता है पर यदि उस शृंखला को ही तोड़ दिया तो उसकी नवीन रचना कठिन होगी।
गायत्री द्वारा आत्मोन्नति होती है यह निश्चित है। मनुष्य के अन्तःक्षेत्र के संशोधन, परिमार्जन, संतुलन एवं विकास के लिए गायत्री से बढ़कर और कोई ऐसा साधन भारतीय धर्म शास्त्रों में नहीं है जो अतीत काल से असंख्यों व्यक्तियों के अनुभवों में सदा खरा उतरता आया हो। मन, बुद्धि चित्त, अहंकार का अन्तःकरण चतुष्टय गायत्री द्वारा शुद्ध कर लेने वाले व्यक्ति के लिए सांसारिक जीवन में सब ओर से, सब प्रकार की सफलताओं का द्वार खुल जाता है। उत्तम स्वभाव अच्छी आदतें, स्वस्थ मस्तिष्क, दूर दृष्टि, प्रफुल्ल मन, उच्च चरित्र, कर्तव्य निष्ठा प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात् गायत्री साधक के लिए संसार में कोई दुःख, कष्टकर नहीं रह जाता, उसके लिए सामान्य परिस्थितियों में भी सुख ही सुख उपस्थित रहता है।
परन्तु गायत्री का यह लाभ केवल 24 अक्षर के मन्त्र मात्र से उपलब्ध नहीं हो सकता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पहिए की गाड़ी नहीं चलती, एक पंख का पक्षी नहीं पड़ता इसी प्रकार अकेली गायत्री साधना अपूर्ण है उसका दूसरा भाग गुरु का पथ प्रदर्शन है। गायत्री गुरु मन्त्र है। इस महा शक्ति की कीलित कुंजी अनुभवी एवं सुयोग्य गुरु के पथप्रदर्शन में सन्निहित है। जब साधक को उभय पक्षीय साधन, गायत्री माता और पिता गुरु की छत्र छाया, प्राप्त हो जाती है तो आशा जनक सफलता प्राप्त होने में देर नहीं लगती।
Versions
-

ENGLISHSuper Science of GayatriScan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानScan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 1Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 2Scan Book Version
-

TELUGUGayatri Mahavigyan Part 3Scan Book Version
-
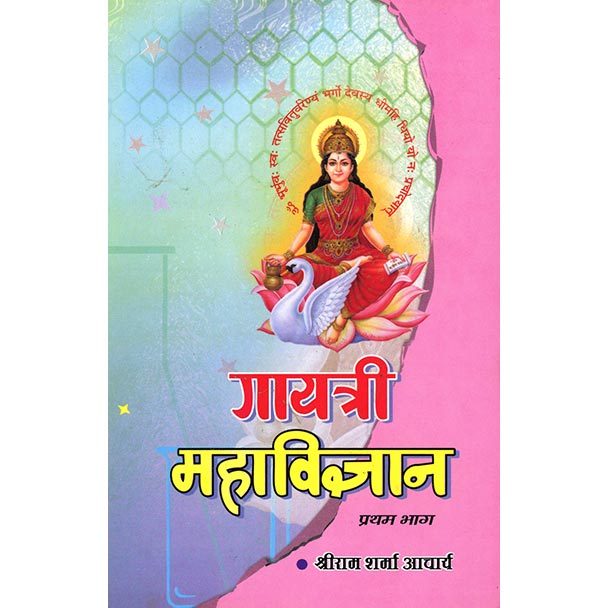
MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग १Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग २Scan Book Version
-

MARATHIगायत्री महाविज्ञान-भाग ३Scan Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञानText Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान (तृतीय भाग)Text Book Version
-

HINDIगायत्री महाविज्ञान भाग 2Text Book Version
Write Your Comments Here:
- गायत्री के पांच मुख
- अनन्त आनन्द की साधना
- अन्नमय कोश की साधना
- उपवास
- आसन
- सूर्य नमस्कार की विधि
- तत्वशुद्धि
- तपश्चर्या
- प्राणमय कोश
- प्राणाकर्षण की सुगम क्रियाएं
- तीन बन्ध
- सात मुद्राएं
- नौ प्राणायाम
- मनोमय कोश
- ध्यान
- त्राटक
- जप साधना
- तन्मात्रा साधना
- शब्द साधना
- रूप साधना
- रस साधना
- गन्ध साधना
- स्पर्श साधना
- विज्ञानमय कोश
- अजपा जाप
- आत्मानुभूति योग
- आत्म चिन्तन की साधना
- स्वर योग
- स्वर बदलना
- स्वर संयम से दीर्घ जीवन
- विज्ञान कोश की वायु साधना
- ग्रन्थि भेद
- आनन्दमय कोश
- नाद साधना
- विन्दु साधना
- कला साधना
- पांच कलाओं तात्विक साधना
- तुरीयावस्था
- पंच कोशी साधना का ज्ञातव्य
- पंच मुखी साधना का उद्देश्य
- गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती
- गायत्री का तन्त्रोक्त वाममार्ग
- गायत्री मंजरी
- गायत्री की रहस्यमयी गुप्त शक्ति
- अनादि गुरु मंत्र गायत्री

