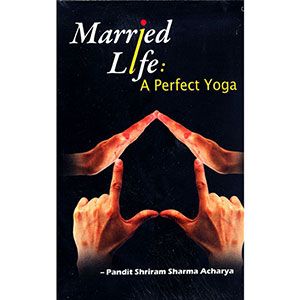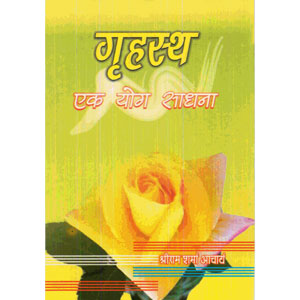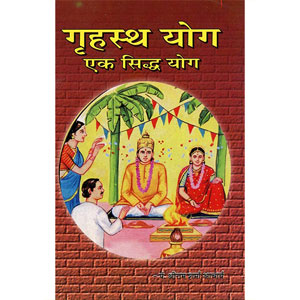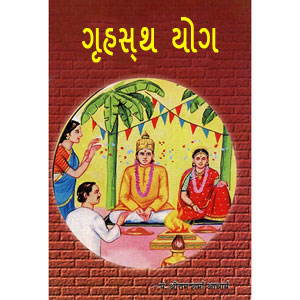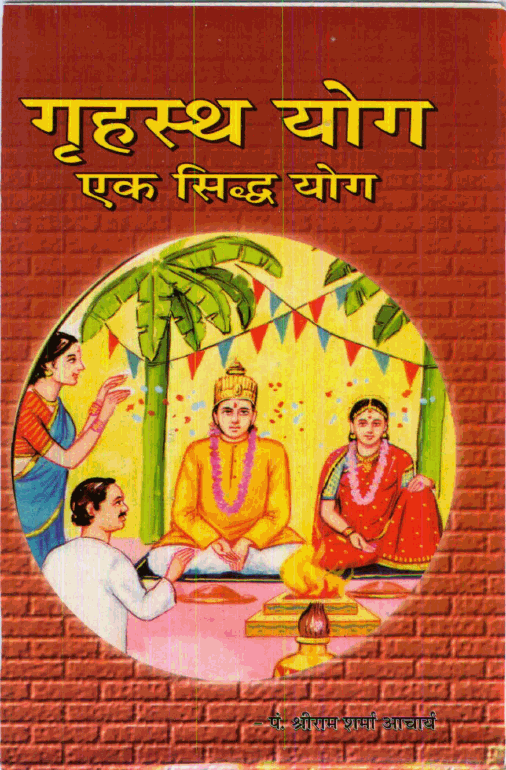गृहस्थ एक योग साधना 
गृहस्थ में वैराग्य
Read Scan Versionगृहस्थ आश्रम की निन्दा करते हुए कोई कोई सज्जन ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि—‘‘घर गृहस्थी में पड़ना माया के बन्धन में फंसना है।’’ उनकी दृष्टि में घर गृहस्थी माया का पिटारा है और बिना गृहस्थी रहना स्वर्ग की निशानी है। परन्तु विचार करने पर प्रतीत होता है कि उपरोक्त कथन कुछ विशेष महत्व का नहीं है कारण यह है कि माया का बन्धन बाहरी वस्तुओं का बाहरी मनुष्यों में नहीं वरन् अपनी मनोवृत्तियों में है यदि मन अपवित्र है, काम, क्रोध, लोभ से भरा हुआ है तो जो बातें गृहस्थ में होती हैं वही संन्यास से बाहर भी हो सकती हैं। हमने देखा है कि बहुत से बाबाजी कहलाने वाले महाराज भिक्षा मांग मांग कर धन जोड़ते हैं, मरने पर उनके पास प्रचुर धनराशि निकलती है। हमने देखा है कि गृह-विहीन लोगों की इन्द्रियां भी लोलुप होती हैं। शब्द, रस, रूप, गन्ध, स्पर्श में वे लोलुप रुचि प्रकट करते हैं, उनके आकर्षण से आकर्षित होते हैं। अपनी वस्तुओं से—कुटी, वस्त्र, पुस्तक, पात्र, शिष्य, साथी आदि से—ममता रखते हैं। यही सब बातें ही दूसरे रूप में गृहस्थों में होती है।
वैराग्य, त्याग, विरक्ति, इन महत्त्वों का सीधा सम्बन्ध अपने मनोभावों से हैं। यदि भावनाएं संकीर्ण हों, कलुषित हों, स्वार्थमयी हों तो चाहे जैसी उत्तम सात्विक स्थिति में मनुष्य क्यों न रहे मन का विकार वहां भी पाप की दुराचार की पुष्टि करेगा। यदि भावनाएं उदार एवं उत्तम हैं तो अनमिन और अनिष्टकारक स्थिति में भी मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता उत्पन्न करेगा। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि ‘‘मुझे नरक में भेज दिया जाय तो मैं वहां अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा।’’ वास्तविक सत्य यही है, हर आदमी अपनी भीतरी स्थिति का प्रतिविम्ब दुनियां के दर्पण में देखता है। यदि उनके मन में माया है, तो घर, बाहर, वन, आरण्य, मन्दिर, स्वर्ग सब जगह माया ही माया है, माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि मन साफ है, पवित्रता, प्रेम और परमार्थ की दृष्टि है तो घर का एक कोना पुनीत तपोवन से किसी भी प्रकार कम न रहेगा। राजा जनक प्रभृति अनेकों ऋषि हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहने की साधना की और परम पद पाया।
वीरता भागने में नहीं, वरन् लड़ने में है। यदि गृहस्थाश्रम में अधिक कठिनाइयां हैं तो उनसे डर कर दूर रहना रचित नहीं। पानी में घुसे बिना तैरना कैसे सीखा जायेगा? कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अखाड़े में जाकर व्यायाम करने की कठिनाई में पड़ना नहीं चाहता, परन्तु पहलवान बनना चाहता हूं, तो उसकी यह बात बालकों जैसी अनगढ़ होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह के दावघातों को देखना, उनसे परिचित होना, उनसे लड़कर विजय प्राप्त करना इन्हीं सब अभ्यासों के लिए वर्णाश्रम धर्म तत्वदर्शी आचार्य गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि आश्रम बताते हैं। सम्पूर्ण देवर्षि इसी महान् गुफा में से उत्पन्न और विकसित हुए हैं। जरा कल्पना तो कीजिये- यदि गृहस्थ धर्म- जिसे निर्बुद्धि लोग माया या बन्धन तक कह बैठते हैं न होता तो राम, कृष्ण, बुद्धि, ईसा, मुहम्मद, गांधी कहां से आते? सीता, सावित्री, अनुसूया, मदालसा, दमयन्ती, पार्वती, आदि सतियों का चरित्र कहां से सुन पड़ता? इतिहास के पृष्ठों पर जगमगाते हुए उज्ज्वल हीरे किस प्रकार दिखाई देते? अन्य तीनों आश्रम बच्चे हैं गृहस्थ उनका पिता है। पिता को बन्धन कहना, नरक बताना त्याज्य ठहराना एक प्रकार की विवेक हीनता है।
उत्तर दायित्व का भार पड़े बिना कोई व्यक्ति वास्तविक, गम्भीर, जिम्मेदार और भारी भरकम नहीं होता। अल्हड़ बछड़े बहुत कूदते फांदते और दुलत्तियां उड़ाते हैं परंतु जब कन्धे पर भार पड़ता है तो बड़ी सावधानी से एक एक कदम रखना पड़ता है। हाथी जब गहरे पानी में धंसता है तो अपना एक पैर भली प्रकार जमा लेता है तब दूसरे को आगे रखता है। उसकी सारी सावधानी और होशियारी उस समय एक स्थान पर केन्द्रीभूत हो जाती है। जिस चित्तवृत्ति निरोध को, एकाग्रता को पातंजलि ने योग बताया है वह एकाग्रता कोरी बातूनी जमावन्दी से नहीं आती, उसके लिये एक प्रेरणा जिम्मेदारी चाहिये। गृहस्थाश्रम का बोझ पड़ने पर मनुष्य जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ाता है। अपना और अपने परिवार का बोझ पीठ पर लाद कर उसे चलना पड़ता है इसलिये उच्छृंखलता को छोड़कर वह जिम्मेदारी अनुभव करता है। यह जिम्मेदारी ही आगे चलकर विवेकशीलता में परिणत हो जाती है। राजा को एक साम्राज्य के संचालन की बागडोर हाथ में लेकर जैसे संभल-संभलकर चलना पड़ता है वैसे ही एक सद्गृहस्थ को पूरी दूरदर्शिता, विचारशीलता, धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम के साथ अपना हर एक कदम उठाना पड़ता है। चाबुक सवार जैसे घोड़े को अच्छी चाल चलना सिखाकर उसे हमेशा के लिये बढ़िया घोड़ा बना देता है वैसे ही गृहस्थ धर्म भी ठोक-पीटकर कड़ुवे-मीठे अनुभव कराकर एक मनुष्य को आत्म-संयमी, दूरदर्शी गम्भीर एवं स्थिर चित्त बना देता है। यह सब योग के लक्षण हैं। जैसे फल पक कर समयानुसार डाली से स्वयं अलग हो जाता है वैसे ही गृहस्थ की डाल से चिपका हुआ मनुष्य धीरे धीरे आत्म निग्रह और आत्म त्याग को शिक्षा पाता रहता है और अन्ततः एक प्रकार का योगी हो जाता है।
लिप्सा, लालसा, तृष्णा, लोलुपता, मदान्धता, अविवेक आदि बातें त्याज्य हैं, यह बुरी बातें गृहस्थ आश्रम में भी हो सकती हैं और आश्रमों में भी। इसीलिये गृहस्थ आश्रम त्यागने योग्य नहीं वरन् अपनी कुवासनाएं ही त्यागने योग्य हैं।