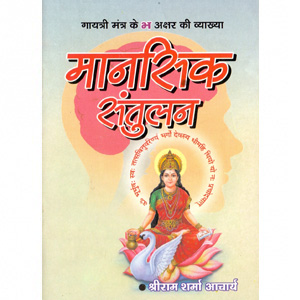मानसिक संतुलन 
मानसिक संतुलन
Read Scan Version
गायत्री मंत्र का नौवाँ अक्षर "भ" हमको प्रत्येक स्थिति में मानसिक भावों को संतुलित रखने की शिक्षा देता है-
अर्थात-''मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ दो । सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो ।''
शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ''ज्वर'' कहलाता है और वह ज्वर अनेक दुष्परिणामों को उत्पन्न करता है । वैसे ही मानसिक ज्वर होने से उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मदहोशी, आतुरता आदि लक्षण प्रकट होते हैं । आवेश की प्रबलता मनुष्य के ज्ञान, विचार, विवेक को नष्ट कर डालती है । उस समय वह न सोचने लायक बातें सोचता है और जो कार्य पहले कुत्सित जान पड़ते थे, उन्हीं को करने लगता है । ऐसी स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा अवांछनीय है । विपत्ति पड़ने पर अथवा किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा हो जाने पर लोग चिंता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध आदि के वशीभूत होकर मानसिक शांति को खो बैठते हैं । इसी प्रकार कोई बड़ी सफलता मिल जाने पर या संपत्ति प्राप्त होने पर मद, मत्सर, अति हर्ष, अति भोग आदि दोषों में फँस जाते हैं । इस तरह कोई भी उत्तेजना मनुष्य की आंतरिक स्थिति को विक्षिप्तों की सी कर देती है । इसके फल से मनुष्य को तरह-तरह के अनिष्ट परिणाम भोगने पड़ते हैं ।
जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी उत्तेजित होने वाली अथवा शीघ्र ही आवेश में आ जाने वाली होती है, वे प्राय: मानसिक निर्बलता के शिकार होते हैं । वे अपने मन को एकाग्र करके किसी एक काम में नहीं लगा सकते और इसलिए कोई बड़ी सफलता पाना भी उनके लिए असंभव हो जाता है । उनके अधिकांश विचार क्षणिक सिद्ध होते हैं । इस प्रकार मानसिक असंतुलन मनुष्य की उन्नति में बाधा स्वरूप बनकर उसे पतन की ओर प्रेरित करने का कारण बन जाता है ।
असंतुलन असफलता का मूल कारण है मानसिक असंतुलन की अशांत दशा में कोई व्यक्ति न तो सांसारिक उन्नति कर सकता है और न आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है । कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊँचा उठने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है; वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्रित नहीं हो पाता ।
जिस प्रकार हाथ काँप रहा हो तो उस समय बंदूक का निशाना नहीं साधा जा सकता, उसी प्रकार आवेश या उत्तेजना की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है । उस उद्विग्नता की दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए ।
मानसिक असंतुलन और उत्तेजना से अधीरता का भाव उत्पन्न होता है । अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बालकपन का चिह्न है । बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली विचित्र होती है। अभी बीज बोया, अभी उसमें खाद-पानी लगाया, अभी दो-चार मिनट के बाद ही बीज को उलट-पलटकर देखते हैं कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं । जब अंकुर नहीं दीखता तो उसे फिर गाड़ देते हैं और दो मिनट बाद फिर देखते हैं । इस प्रकार कई बार देखने पर भी जब वृक्ष उत्पन्न होने की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय काम में लाते हैं । वृक्षों की टहनियों तोड़कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे बाग की लालसा को बुझाने का प्रयत्न करते हैं । उन टहनियों के पत्ते उठा-उठाकर देखते हैं कि फल लगे या नहीं। यदि दस-बीस मिनट में फल नहीं लगते तो कंकडों को डोरे से बाँधकर टहनियों में लटका देते हैं। इस अधूरे बाग से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती । फलतः कुछ देर बाद उस बाग को बिगाड़कर चले जाते हैं । कितने ही जवान और वृद्ध पुरुष भी उसी प्रकार की बाल-क्रीड़ाएँ अपने क्षेत्र में किया करते हैं, किसी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं, इस ''उत्साह'' की अति उतावली बन जाती है। कार्य आरंभ हुए देर नहीं होती कि यह देखने लगते हैं कि सफलता में अभी कितनी देर है । जस भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती । जब उन्हें थोड़े ही समय में रंगीन कल्पनाएँ पूरी होती नहीं दीखतीं तो निराश होकर उसे छोड़ बैठते हैं । अनेक कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़नी, ऐसी ही बाल-क्रीड़ाएँ वे जीवन भर करते रहते हैं । छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छापूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते, इन बाल-क्रीड़ा करने वाले अधीर पुरुषों की भी मनोभूमि ऐसी ही होती है । यदि हथेली पर सरसों न जमी तो खेल बिगाड़ते हुए उन्हें देर नहीं लगती ।
प्राचीन समय में जब शिष्य विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था तो उसे पहले अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती थी । गौएँ चरानी पड़ती थीं, लकड़ियाँ चुननी पड़ती थीं, उपनिषदों में इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं । इंद्र को भी लंबी अवधि तक इसी प्रकार तपस्यापूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, जब वह अपने धैर्य की परीक्षा दे चुका, तब उसे आवश्यक विद्या प्राप्त हुई ।
प्राचीन काल में विज्ञपुरुष जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को ही विद्याध्ययन कराते थे । क्योंकि उनके पढ़ाने का परिश्रम भी अधिकारी छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था । चंचल चित्त वाले, अधीर स्वभाव के मनुष्य का पढ़ना न पढ़ना बराबर है । अक्षरज्ञान हो जाने या अमुक कक्षा का सर्टिफिकेट ले लेने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ।
आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है । कर्म को परिपक्व होने में समय लगता है । रूई को कपड़े के रूप तक पहुँचने के लिए कई कड़ी मंजिलें पार करनी होती हैं और कठोर व्यवधानों में होकर गुजरना पड़ता है, जो संक्रांति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक पूरा होने देने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रूई को कपड़े के रूप में देखने की आशा न करनी चाहिए। किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा फल बनता है । इसमें देर लगती है और कठिनाई भी आती है । कभी-कभी परिस्थितिवश यह देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है । उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है । कभी-कभी तो कई बार का प्रयत्न भी सफलता तक नहीं ले पहुँचता, तब अनेक बार अधिक समय तक अविचल धैर्य के साथ जुटे रहकर अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करना होता है ।
आतुर मनुष्य इतनी दृढ़ता नहीं रखते, जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं । यही भगोड़ापन उनकी पराजयों का इतिहास बनता जाता है ।
चित्त का एक काम पर न जमना, संशय और संकल्प-विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है । यदि काम पूरा न हो पाया तो ? यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई तो ? यदि फल उलटा निकला तो ? इस प्रकार की दुविधापूर्ण आशंकाएँ मन को डाँवाडोल बनाए रहती हैं ।
पूरा आकर्षण और विश्वास न रहने के कारण मन उचटा-उचटा सा रहता है । जो काम हाथ में लिया हुआ है, उस पर निष्ठा नहीं होती । इसलिए आधे मन से वह किया जाता है । आधा मन दूसरे काम की खोज में लगा रहता है । इस डाँवाडोल स्थिति में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता । हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती । बल्कि उलटी भूल होती जाती है, ठोकर पर ठोकर लगती जाती हैं । दूसरी ओर आधे मन से जो नया काम तलाश किया जाता है, उसके हानि-लाभों को भी पूरी तरह नहीं विचारा जा सकता । अधूरी कल्पना के आधार पर नया काम वास्तविक रूप में नहीं, वरन आलंकारिक रूप में दिखाई पड़ता है । पहले काम को छोड़कर नया पकड़ लेने पर फिर उस नए काम की भी वही गति होती है जो पुराने की थी । कुछ समय बाद उसे भी छोड़कर नया ग्रहण करना पड़ता है । इस प्रकार ''काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना'' इस कार्यक्रम की बराबर पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य को अपने असफल जीवन पर पश्चात्ताप करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता ।
मानसिक असंतुलन में आध्यात्मिक पतन मानसिक असंतुलन से केवल सांसारिक और भौतिक क्षेत्र में ही हानि नहीं उठानी पड़ती, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका परिणाम अनिष्टकारी होता है । जो लोग मानसिक उत्तेजना के शीघ्र वशीभूत हो जाते हैं, उनमें अभिमान और लोभ की मात्रा भी बढ़ जाती है और ये दोनों तत्व अन्य अनेक प्रकार के दोषों की उत्पत्ति करते हैं । अभिमान एक प्रकार का नशा है, जिसमें मदहोश होकर मनुष्य अपने को दूसरों से बड़ा और दूसरों को अपने से छोटा समझता है । वह इस बात को पसंद करता है कि दूसरे लोग उसकी खुशामद करें, उसे बड़ा समझें, उसकी बात मानें, जब इसमें कुछ कमी आती है तो वह अपना अपमान समझता है और क्रोध से साँप की तरह फुफकारने लगता है । वह नहीं चाहता कि कोई मुझसे धन में, विद्या में, बल में, प्रतिष्ठा में बज या बराबर का हो, इसलिए जिस किसी को वह थोड़ा सुखी-संपन्न देखता है उसी से ईर्ष्या-द्वेष करने लगता है । अहंकार की पूर्ति के लिए अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहता है । संपन्नता सद्गुणों से, श्रम से, लगातार परिश्रम करने से मिलती है, पर अभिमान के नशे में चूर व्यक्ति सीधे-साधे मार्ग पर चलने में समर्थ नहीं होता, वह अनीति और बेईमानी पर उतर आता है ।
अवमान का अर्थ है-आत्मा की गिरावट । अपने को दीन, तुच्छ, अयोग्य, असमर्थ समझने वाले लोग संसार में दीन-हीन बनकर रहते हैं ।
उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है । कोई साहसिक कार्य उनसे बन नहीं पड़ता । संपन्नता प्राप्त करने और अपने ऊपर होने वाले अन्याय को हटाने के लिए जिस शौर्य की आवश्यकता है, वह अवमानग्रस्त मनुष्य में नहीं होता । फलस्वरूप वह न तो समृद्ध बन पाता है और न अन्याय के चंगुल से छूट पाता है । उसे गरीबी घेरे रहती है और कोई न कोई सताने वाला आए दिन अपनी तीर कमान ताने रहता है । इन कठिनाइयों से बचने के लिए उसे निर्बलतापूर्वक अनीतियों का आश्रय लेना पड़ता है । चोरी, ठगी, कपट, छल, दंभ, असत्य, पाखण्ड, व्यभिचार, खुशामद जैसे दीनता सूचक अपराधों को करना पड़ता है । मोह-ममता, भय-आशंका, चिंता-कातरता, शोक-पश्चात्ताप, निराशा-कुढ़न सरीखे मनोविकार उसे घेरे रहते हैं । आत्मज्ञान एवं आत्मसम्मान को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्योचित मार्ग अपनाना, यह जीवन का सतोगुणी स्वाभाविक क्रम है । यह शृंखला जब विशृंखलित हो जाती है, आत्मिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो पाप करने का सिलसिला चल पड़ता है ।
मानसिक संतुलन और समत्व की भावना मानसिक संतुलन को हम गीता में बतलाई समत्व की भावना भी कह सकते हैं । सब सांसारिक पदार्थों में प्रवृत्ति की हम में जितनी शक्ति होती है, उतनी ही जब उनसे निवृत्त होने की भी शक्ति होती है, तो उस अवस्था को संतुलित और समत्व भावना की अवस्था कह सकते हैं ।
इस समत्व को आचरण में उतारने के लिए केवल विरागी अथवा रागहीन होने से ही कार्य न चलेगा । संतुलित अवस्था तो तब होगी, जब आप रणहीन होने के साथ-साथ द्वेषहीन भी होंगे । हमारे भारतीय साधुओं ने भी वही भूल की । वे होने के लिए तो विरागी हो गए, पर साथ साथ अद्वेषी (अद्वेष्टा) न हुए । राग से बचने की धुन में उन्होंने द्वेष को अपना लिया । संसार के सुख-दुःख से संबद्ध न होने की चाह में उन्होंने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और उसकी सेवाओं से अपना मुख मोड़ लिया ।
जब दो गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवृत्त करते हैं, तो उनके पारस्परिक संयोग से चित्त की जो अवस्था होती है, उसे ही संतुलित अवस्था कहते हैं । दया मनुष्य को दूसरों का दु:ख दूर करने में प्रवृत्त कराती है, पर निर्मोह या निर्ममत्व मनुष्य को दूसरों के सुख-दु:ख से संबंधित होने से पीछे हटाता है। अतएव दया और निर्ममत्व दोनों के एक बराबर होने से चित्त संतुलित होता है । जहाँ दया मनुष्य को अनुरक्त करती है, वहाँ निर्ममता विरक्त । दया में प्रवृत्तात्मक और निर्ममता में निवृत्तात्मक शक्ति है । उसी तरह संतोष और परिश्रमशीलता एकदूसरे को संतुलित करते हैं । परिश्रमशीलता में प्रवृत्तात्मक और संतोष में निवृत्तात्मक शक्ति है । उसी तरह सत्यता और मृदुभाषिता, सरलता और दृढ़ता, विनय और निर्भीकता, नम्रता और तेज, सेवा और अनासक्ति, शुचिता और घृणाहीनता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, तितिक्षा और आत्मरक्षा, निष्कामता और आलस्यहीनता, अपरिग्रह और द्रव्योपार्जन शक्ति परस्पर एकदूसरे को संतुलित करते हैं । इन युग्मों में से यदि केवल एक का ही विकास हो और दूसरे के विकास की ओर ध्यान न दिया जाए तो मनुष्य का व्यक्तित्व असंतुलित एवं एकांगी हो जाएगा । श्रद्धालु व्यक्ति में श्रद्धेय व्यक्ति का अनुगमन करने तथा उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है, स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति पर अंकुश न होने से उसमें निरंकुशता और उच्छृंखलता बढ़ सकती है, दृढ़ प्रकृति व्यक्ति में हठ करने की प्रवृत्ति हो सकती है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति में अभिमान बढ़ सकता है, इत्यादि ।
अतएव जब तक इन व्यक्तियों में क्रमश: आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व, हठहीनता और निरभिमानता का विकास न होगा, तब तक पूर्वोक्त गुण अपनी-अपनी सीमा के भीतर न रहेंगे । अतएव उपरोक्त युग्मों में से प्रत्येक गुण एकदूसरे को मर्यादित करता है और एकदूसरे का पूरक है ।
जब मनुष्य में दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी अपमान सहन करने की क्षमता होती है, जब वह अहिंसा व्रत पालते हुए भी अपराधियों को अधिकाधिक उच्छृंखल, उद्धत, अभिमानी और निष्ठुर नहीं बनने देता, जब वह सेवाव्रती होते हुए भी सेव्यजनों को आलसी, परमुखापेक्षी और अकर्मण्य नहीं होने देता, जब वह क्रोध में होते हुए भी अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना जानता है, जब उसमें भक्ति और उत्साह होते हुए भी दासवृत्ति और उतावलापन नहीं होता, जब वह सफलता में विश्वास रखते हुए भी कार्य करने में लापरवाही नहीं करता, जब वह त्यागी होते हुए भी विपक्षी का लोभ नहीं बढ़ाता, जब वह मान-सम्मान की परवाह न करते हुए भी लोक-कल्याण करने वाले शुभ कार्यों के करने में पूर्ण उत्साही होता है, जब वह अपमान से दुखी न होते हुए भी अपमानजनक कार्य न करने का संयमी एवं आत्मनिग्रही होता है, जब वह शुभ कर्मों को करने के लिए बाध्य न होते हुए भी स्वेच्छा से उन्हें तत्परतापूर्वक अच्छी तरह करता है, जब वह किसी कार्य में प्रवृत्त होने के साथ-साथ उससे निवृत्त भी हो सकता है, तब उसके चरित्र और गुणावलियों में संतुलन आता है ।
जब दो विचारधाराएँ मनुष्य से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य कराती हैं, तब उनके समन्वय से जो स्थिति होती है, उसे संतुलित विचारधारा कहते हैं । आत्मसुख की भावना बहुधा मनुष्य को स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त कराती है और लोकसुख की भावना लोक-कल्याण के कार्यों में । अतएव आत्मसुख और लोकसुख दो विभिन्न दृष्टिकोण हुए । इनके समन्वय से जो स्थिति होती है, वही संतुलित विचारपद्धति है । उसी प्रकार जिसकी विचारधारा में पूर्व और पश्चिम के आदर्शों का समन्वय, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, आदर्श और यथार्थ का समन्वय हुआ है और जो मध्यम मार्ग को अपनाए हुए है, उसी की विचारधारा संतुलित है । जब हम किसी एक ही कार्य के पीछे पड़ जाते हैं अथवा हम जब किसी कार्य में अति करने के कारण दूसरे करणीय कार्यों को भूल जाते हैं, तब हमारी कार्यपद्धति असंतुलित होती है । यदि हम एकदम धन कमाने के पीछे पड़ जाएँ अथवा यदि हम केवल पढ़ने में ही सारा समय बिताने लगें तो हमारी कार्यपद्धति असंतुलित होगी । यदि कोई विद्यार्थी अपने हस्तलेखन की केवल गति ही बढ़ाने पर ध्यान दे और अक्षरों की सुंदरता पर ध्यान न दे तो आप उसके प्रयत्न को क्या कहेंगे ? उसी प्रकार यदि किसी देश में ऐसा कोई आयोजन हो कि केवल शिक्षा की क्वालिटी या उसकी उत्कृष्टता ही एकमात्र लक्ष्य हो और इस बात का ध्यान न हो कि शिक्षा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपलब्ध हो सके तो उस देश के शिक्षाशास्त्रियों की कार्यपद्धति असंतुलित ही कही जाएगी । यही बात मानव जीवन पर भी घटित होती है । हमें केवल एक ही दिशा में घुड़दौड़ नहीं मचानी चाहिए, वरन सब दिशाओं में विकास करते हुए मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए । तभी हम अगाध मानसिक शांति के दर्शन कर सकेंगे ।
'अति सर्वत्र वर्जयेत' हमारे प्राचीन शास्त्रकारों तथा नीतिकारों ने जगह-जगह इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी काम में ''अति'' नहीं करनी चाहिए । यह नियम बुरी बातों पर ही नहीं अनेक अच्छी बातों पर भी लागू होता है ।
जैसे कहा गया है कि अति दानवृत्ति के कारण बलि को पाताल में बँधना पड़ा । संभव है कि कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए जो किसी असाधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं, यह नियम आवश्यक न माना जाए, पर सर्वसाधारण के लिए सदैव मध्यम मार्ग-संतुलित जीवन का नियम ही उचित सिद्ध होता है ।
भगवान बुद्ध ने ''मज्झम मग्ग'' का, मध्यम मार्ग का, आचरण करने के लिए सर्वसाधारण को उपदेश किया है । बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे-धीरे चलने वाले अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचने में पिछड़ जाते हैं । जो मध्यम गति से चलता है, वह बिना थके, बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है ।
पानी में डूब सकता है, किसी दल-दल में फँस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुँह पटक खाकर प्राण गँवा सकता है । साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का कार्य न करे पानी की विस्तृत धारा को देख कर डर जाय तो नदी पार नहीं कर सकता । हाथी बुद्धिमान प्राणी है । वह अपने भारी भरकम डीलडौल का स्थान रखता है नदी पार करने की आवश्यकता अनुभव करता है पानी के विस्तृत फैलाव को समझता है । इन सब बातों का आन रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरता पूर्वक आरम्भ करता है । जहाँ खतरा दीखता है वहाँ से पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह होकर रास्ता ढूँढ़ता है । इस प्रकार वह अपना कार्य पूरा कर लेता है । मनुष्य को भी हाथी की सी बुद्धिमानी सीखनी चाहिए और अपने कार्यों को मध्यम गति से पूरा करना चाहिए । विद्यार्थी कितनी ही उतावली करे एक दो महीने में अपनी शिक्षा पूरी कर नहीं सकता कर भी लेगा तो उसे जल्दी भूल जायगा । क्रम-क्रम से नियतकाल में पूरी हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है । पेड़ पौधे वृक्ष पशु-पक्षी सभी अपनी नियत अवधि में परिपक्व फल देने लायक तथा वृद्ध होते है यदि उस नियति गति विधि में जल्दबाजी की जाय तो परिणाम बुरा होता है । हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता मनोभूमि परिस्थिति आदि को यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूरा करना चाहिए ।
बहुत खाना भूख से ज्यादा खाना बुरा है- इसी प्रकार बिल्कुल न खाना-भूखे रहना बुरा है । अति का भोग मृत है पर अमर्यादित तप भी बुरा है । अधिक विषयी क्षीण हो कर असमय में ही मर जाते है पर जो अमर्यादित अतिशय तप करते है शरीर को अत्यधिक कस डालते हैं वे भी दीर्घ जीवी नहीं होते । अति का कंजूस होना ठीक नहीं पर इतना दानी होना भी किस काम का कि कल खुद को ही दाने-दाने का मुँहताज बनना पड़े । आलस्य में पड़े रहना हानि कारक है पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रह कर जीवनी शक्ति को समाप्त कर डालना भी लाभदायक नहीं । कुबेर बनने की तृष्णा में पागल बन जाना या कंगाली में दिन काटना दोनों ही स्थितियाँ अवांछनीय हैं । नित्य मिठाई ही खाने को मिले तो उससे अरुचि के साथ-साथ दस्त भी शुरू हो जायेंगे । भोजन में मीठे की मात्रा बिल्कुल न हो तो चमड़ी पीली पड़ जायगी । बहुत घी खाने से मन्दाग्नि हो जाती है पैर यदि बिल्कुल घी न मिले तो खून खराब हो जायेगा । बिल्कुल कपड़े न हो तो सर्दी में निमोनिया हो जाने का और गर्मी में लू लग जाने का खतरा है पर, जो कपड़ों के परतों से बेतरह लिपटे रहते हैं उनका शरीर आम की तरह पीला पड़ जाता है । बिल्कुल न पढ़ने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता पर दिन रात पढ़ने की धुन में व्यस्त रहने से दिमाग खराब हो जाता है, आँखें कमजोर पड़ जाती हैं ।
घोर, कट्टर, असहिष्णु, सिद्धान्तवादी बनने से काम नहीं चलता । दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है । अन्य भक्त बनना या अविश्वासी होना दोनों ही बातें बुरी हैं । विवेक पूर्वक हंस की भांति नीर क्षीर का अन्वेषण करते हुए प्राण और अग्राह्य को प्रथक करना ही बुद्धिमानी है । देश काल और पात्र के भेद से नीति व्यवहार और क्रिया पद्यति में भेद करना पड़ता है ।
यदि न करें तो हम अतिवादी कहे जायेंगे । अतिवादी-आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं पर नेतृत्व नहीं कर सकते ।
आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी प्रगति उसी ओर होनी चाहिए, पर सावधान! कहीं अपरिपक्व अवस्था में ऐसी बड़ी छलांग न लगाई जाय जिसके परिणाम स्वरूप टांग टूटने की यातना सहनी पड़े । कड़े कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है । मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवानों का होता है । उतावली करने वाले छछोरे या रेंगने वाले आलसी नहीं महत्त्वपूर्ण सफलतायें वे प्राप्त करते है जो धैर्यवान होते हैं जो विवेक पूर्वक मजबूत कदम उठाते हैं और जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते है ।
नियमितता, दृढ़ता एवं स्थिरता के साथ समगति से कार्य करते रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही उपयोगी संतुलित कार्यों का सम्पादन होता है ।
एकांगी विकास की हानियाँ मानसिक असंतुलन से मनुष्य के व्यक्तित्व का एकांगी विकास होता है । हममें से प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से नई परिस्थितियों में फिट होने का प्रयत्न करता रहता है । यदि हम अपने, घर, पेशे वातावरण के अनुसार अपने मानसिक संस्थान को ढक लेते हैं तो हमें कार्य में प्रसन्नता और मन में शान्ति प्राप्त होती है । अन्यथा हमारा मन अतृप्त और हमारी आत्मा अशान्त रहती है ।
उदाहरण स्वरूप कुछ ऐसे विचार और तथ्य होते हैं जिनके प्रति हम ईर्ष्यालु हो उठते हैं । हम इन विचारों से बच नहीं सकते । उनके बावजूद हमें इन्हीं विरोधी विचारों में कार्य करना है उनसे मित्रता करनी है । तभी हमें मानसिक शान्ति प्राप्त हो उठेगी ।
मन में आन्तरिक संघर्ष का क्या कारण है ? दो विरोधी विचार, दो विभिन्न दृष्टिकोण हमारे मानसिक क्षितिज पर उदित होते हैं । हमें इन दोनों के बाबजूद कार्य करना है । संतुलन ही शान्ति का एक मात्र उपाय है ।
चोरी करने वाला व्यक्ति वह है जो अपने विचार भावना और अन्तरात्मा में पारस्परिक संतुलन नहीं कर पोता । उसकी लालच और मोह की प्रवृत्ति अन्तरात्मा को दबा देती है । वह मोह को लम्बा छोड़ देता है और स्वयं भी उसमें लिपट जाता है । सत्य और न्याय की पुकार दब जाती है । पापमयी वृत्ति की विजय होती है । शैतान बच्चे झगड़ालू औरतें, सब इस मानसिक रोग के शिकार होते हैं । वे मानसिक जगत को ठीक तरीके से संचालित और संतुलित नहीं कर पाते हैं । कोई विकार इतना तीव्र हो जाता है जो विवेक बुद्धि को दबाकर उनके स्वभाव का एक अंग बन जाता है । मन की क्रियाओं को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, १-भावना २-विचार ३-क्रियायें । ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनमें उपरोक्त तीनों क्रियाओं का पूर्ण सामन्जस्य या पूर्ण संतुलन हो । किसी में भावना का अंश अधिक है तो वह भावुकता से भरा है आवेशों को विचार रहता है । उसकी कमजोरी-अति संवेदन शीलता है । वह जरा सी भावना को तिल का ताड़ बनाकर देखता है ।
विचार प्रधान व्यक्ति दर्शन की गुड़ गुत्थियों में ही डूबते उतराते रहते हैं । नाना कल्पनाऐं उनके मानस क्षितिज पर उदित अस्त होती रहतीं है । योजना बनाने का कार्य उनसे खूब करा लीजिए । पर असली काम के नाम वे शून्य हैं ।
तीसरे प्रकार के व्यक्ति सोचते कम हैं भावना में नहीं बहते हैं पर काम खूब करते रहते हैं । इन कार्यों में ऐसे भई काम वे कर डालते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती तथा जिनके बिना भी उनका काम चल सकता है । पूर्ण संतुलित वही व्यक्ति है जिसमें भावना विचार तथा कार्य इन तीनों ही तत्वों का पूर्ण सामंजस्य या मेल हो । ऐसा व्यक्ति मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ है । हमें चाहिए कि हम अति से अपनी रक्षा करें और इस प्रकार असंतुलन से बचे रहे । कहने का तात्पर्य यह है कि अति भावुकता के चक्र में पड़ कर ऐसा न कर डाले ऐसे वायदे न कर बैठें जिन्हें बाद में पूर्ण न कर सकें । इतने विचार-प्रधान न बन जायें कि सम्पूर्ण समय सोचते विचारते चिन्तन करते-करते ही व्यतीत हो जाय । विचार करना उचित हैं किन्तु विचारों ही में निरन्तर डूबे रहना और कार्य न करना हमें मानसिक रूप से आलसी बना डालेगा ।
अच्छे व्यक्ति के निर्माण में क्रिया भावना, तथा विचार शक्ति इन तीनों आवश्यक तत्वों का पूर्ण विकास होना चाहिए । जो व्यक्ति काम क्रोध आवेश उद्वेग इत्यादि में निरत रहते हैं उन्हें भावनाजन्य मानसिक व्याधियों का परित्याग करना चाहिए । जो केबल कागजी योजना से और व्योम-विहारिणी कल्पनाओं में लगे रहते हैं, इन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से अपनी योजनाओं की सत्यता जांचनी चाहिए । इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अपने कार्यों को जीवन में प्रकट करना चाहिए । हम महान पुरुषों में देखते हैं कि उनकी बुद्धि पूर्ण विकास को पहुँच चुकी थी, विचार और इच्छा शक्ति बड़ी बलवती थी और कार्य शक्ति उच्चकोटि की थी । महात्मा गाँधी ऐसे संतुलित व्यक्तित्व के उदाहरण थे ।
जीवन में संतुलन का महत्त्व एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हवा के भयंकर तूफान में चला जा रहा है । धूल से उसके नेत्र क्षण भर के लिए बन्द हो जाते हैं । अधिमिचे नेत्रों से वह दूसरी ओर बहक जाता है । ठीक मार्ग पर आरुढ़ होना चाहता है किन्तु मार्ग नहीं सूझता ।
यही हाल मानव के अन्तर्जगत का है । वह अन्दर ही अन्दर अनेक विरुद्ध भावनाओं का शिकार रहता है । प्रलोभन का मायाजाल और वासना की आँधी उसे घेरे रहती है और वासना तृप्ति के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है । उसे पथ भ्रष्ठ होते देख उसकी शुभ शक्तियां उसे सचेत करती हैं । यदि उनकी शक्ति अधिक हो तो व्यक्ति बच जाता हैं, अन्यथा पतन के गर्त में विलीन हो जाता हैं ।
मानव जीवन में अनेक आन्तिरिक एवं बाह्य शक्तियों का प्राधान्य है । भावना कहती है-
''अमुक व्यक्ति बड़ी दयनीय स्थिति में है । उसकी सहायता करें, अपने सुख सुविधा, साधनों को न देखें । कर्ण, शिवि, राजा हरिश्चन्द्र का उदाहरण लीजिए । इन महापुरुषों ने दया करुणा सहानुभूति और दान द्वारा महान पद प्राप्त किया । हमें भी यही करना चाहिए । अपने सुख सुविधा इत्यादि का कोई आन न रखना चाहिए ।'' तर्क आपको रोकता है और कहता है- ''क्या पागल हुए हो सोचो विचारों दिमाग से काम लो । यदि साधनों का ध्यान छोड़कर व्यय किया दूसरों से बड़े बड़े वायदे किए तो आफत में फँस जाओगे । भावना में मत बहो । समाज रुपये का आदर करता है ।'' विलास भावनाऐं कहती हैं- "अरे मानव तूने बहुत श्रम कर" लिया है । अब कुछ आनन्द मना ले । जीवन का रस ले । बार-बार जीवन आने वाला नहीं है ।"
इस प्रकार मानव के आन्तरिक जीवन में भावना तर्क वासना शरीर बल, आत्म बल, प्रेम द्वेष, घृणा इत्यादि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का अविराम ताण्डव चलता रहता है । जो इन शक्तियों का उचित समन्वय कर सकता है वही सफल है । जीवन में भावना की आवश्यकता है बिना भावना का मनुष्य मिट्टी या पत्थर का पुतला मात्र बन जाता है । तर्क अर्थात् विवेक की आवश्यकता भी है । जो सोच समझ कर कार्य न करे, बुद्धि से काम न ले वह तो निराट पशु ही है । इसी प्रकार वासना, घृणा, प्रेम इत्यादि सबका अपने अपने स्थान पर महत्त्व है । पर सुख और सफलता मानव की विभिन्न शक्तियों के संतुलन में ही है । असंतुलन में पराजय छिपी हुई है ।
सिकन्दर महान, जूलियस सीजर और औरंगजेब की अत्यंत बड़ी महत्त्वाकांक्षाओं का परिणाम हमारे सामने है । कर्ण के पतन का कारण अति भावुकता थी, रावण दर्प के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ । तर्कशील, भावनाशील, कर्मशील-तीनों ही प्रकार के मानव जीवन में अमर्यादित संतुलन से असफल हो सकते हैं । इसलिए यह ध्यान रखें कि कहीं आपके व्यक्तित्व का एक ही पहलू विकसित न होता रहे । सभी संतुलित रूप में विकसित होते रहें । अतिरेक त्याज्य है । ध्येय और व्यवहार कर्म और भावना, परिश्रम और विश्राम तर्क और कार्य इन सभी द्वन्द्वों में उचित समन्वय का नाम ही जीवन है ।
भ-भवोद्विग्नमना नैव हदुद्वेगं परित्यज ।
कुरु सर्वास्ववस्थासु शांतं संतुलित मन: ।
कुरु सर्वास्ववस्थासु शांतं संतुलित मन: ।
अर्थात-''मानसिक उत्तेजनाओं को छोड़ दो । सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो ।''
शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ''ज्वर'' कहलाता है और वह ज्वर अनेक दुष्परिणामों को उत्पन्न करता है । वैसे ही मानसिक ज्वर होने से उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मदहोशी, आतुरता आदि लक्षण प्रकट होते हैं । आवेश की प्रबलता मनुष्य के ज्ञान, विचार, विवेक को नष्ट कर डालती है । उस समय वह न सोचने लायक बातें सोचता है और जो कार्य पहले कुत्सित जान पड़ते थे, उन्हीं को करने लगता है । ऐसी स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा अवांछनीय है । विपत्ति पड़ने पर अथवा किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा हो जाने पर लोग चिंता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध आदि के वशीभूत होकर मानसिक शांति को खो बैठते हैं । इसी प्रकार कोई बड़ी सफलता मिल जाने पर या संपत्ति प्राप्त होने पर मद, मत्सर, अति हर्ष, अति भोग आदि दोषों में फँस जाते हैं । इस तरह कोई भी उत्तेजना मनुष्य की आंतरिक स्थिति को विक्षिप्तों की सी कर देती है । इसके फल से मनुष्य को तरह-तरह के अनिष्ट परिणाम भोगने पड़ते हैं ।
जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी उत्तेजित होने वाली अथवा शीघ्र ही आवेश में आ जाने वाली होती है, वे प्राय: मानसिक निर्बलता के शिकार होते हैं । वे अपने मन को एकाग्र करके किसी एक काम में नहीं लगा सकते और इसलिए कोई बड़ी सफलता पाना भी उनके लिए असंभव हो जाता है । उनके अधिकांश विचार क्षणिक सिद्ध होते हैं । इस प्रकार मानसिक असंतुलन मनुष्य की उन्नति में बाधा स्वरूप बनकर उसे पतन की ओर प्रेरित करने का कारण बन जाता है ।
असंतुलन असफलता का मूल कारण है मानसिक असंतुलन की अशांत दशा में कोई व्यक्ति न तो सांसारिक उन्नति कर सकता है और न आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है । कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊँचा उठने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है; वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्रित नहीं हो पाता ।
जिस प्रकार हाथ काँप रहा हो तो उस समय बंदूक का निशाना नहीं साधा जा सकता, उसी प्रकार आवेश या उत्तेजना की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है । उस उद्विग्नता की दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए ।
मानसिक असंतुलन और उत्तेजना से अधीरता का भाव उत्पन्न होता है । अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बालकपन का चिह्न है । बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली विचित्र होती है। अभी बीज बोया, अभी उसमें खाद-पानी लगाया, अभी दो-चार मिनट के बाद ही बीज को उलट-पलटकर देखते हैं कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं । जब अंकुर नहीं दीखता तो उसे फिर गाड़ देते हैं और दो मिनट बाद फिर देखते हैं । इस प्रकार कई बार देखने पर भी जब वृक्ष उत्पन्न होने की उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय काम में लाते हैं । वृक्षों की टहनियों तोड़कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे बाग की लालसा को बुझाने का प्रयत्न करते हैं । उन टहनियों के पत्ते उठा-उठाकर देखते हैं कि फल लगे या नहीं। यदि दस-बीस मिनट में फल नहीं लगते तो कंकडों को डोरे से बाँधकर टहनियों में लटका देते हैं। इस अधूरे बाग से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती । फलतः कुछ देर बाद उस बाग को बिगाड़कर चले जाते हैं । कितने ही जवान और वृद्ध पुरुष भी उसी प्रकार की बाल-क्रीड़ाएँ अपने क्षेत्र में किया करते हैं, किसी काम को बड़े उत्साह से आरंभ करते हैं, इस ''उत्साह'' की अति उतावली बन जाती है। कार्य आरंभ हुए देर नहीं होती कि यह देखने लगते हैं कि सफलता में अभी कितनी देर है । जस भी प्रतीक्षा उन्हें सहन नहीं होती । जब उन्हें थोड़े ही समय में रंगीन कल्पनाएँ पूरी होती नहीं दीखतीं तो निराश होकर उसे छोड़ बैठते हैं । अनेक कार्यों को आरंभ करना और उन्हें बिगाड़नी, ऐसी ही बाल-क्रीड़ाएँ वे जीवन भर करते रहते हैं । छोटे बच्चे अपनी आकांक्षा और इच्छापूर्ति के बीच में किसी कठिनाई, दूरी या देरी की कल्पना नहीं कर पाते, इन बाल-क्रीड़ा करने वाले अधीर पुरुषों की भी मनोभूमि ऐसी ही होती है । यदि हथेली पर सरसों न जमी तो खेल बिगाड़ते हुए उन्हें देर नहीं लगती ।
प्राचीन समय में जब शिष्य विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था तो उसे पहले अपने धैर्य की परीक्षा देनी होती थी । गौएँ चरानी पड़ती थीं, लकड़ियाँ चुननी पड़ती थीं, उपनिषदों में इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं । इंद्र को भी लंबी अवधि तक इसी प्रकार तपस्यापूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, जब वह अपने धैर्य की परीक्षा दे चुका, तब उसे आवश्यक विद्या प्राप्त हुई ।
प्राचीन काल में विज्ञपुरुष जानते थे कि धैर्यवान पुरुष ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए धैर्यवान स्वभाव वाले छात्रों को ही विद्याध्ययन कराते थे । क्योंकि उनके पढ़ाने का परिश्रम भी अधिकारी छात्रों द्वारा ही सफल हो सकता था । चंचल चित्त वाले, अधीर स्वभाव के मनुष्य का पढ़ना न पढ़ना बराबर है । अक्षरज्ञान हो जाने या अमुक कक्षा का सर्टिफिकेट ले लेने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ।
आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है । कर्म को परिपक्व होने में समय लगता है । रूई को कपड़े के रूप तक पहुँचने के लिए कई कड़ी मंजिलें पार करनी होती हैं और कठोर व्यवधानों में होकर गुजरना पड़ता है, जो संक्रांति काल के मध्यवर्ती कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक पूरा होने देने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे रूई को कपड़े के रूप में देखने की आशा न करनी चाहिए। किया हुआ परिश्रम एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा फल बनता है । इसमें देर लगती है और कठिनाई भी आती है । कभी-कभी परिस्थितिवश यह देरी और कठिनाई आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है । उसे पार करने के लिए समय और श्रम लगाना पड़ता है । कभी-कभी तो कई बार का प्रयत्न भी सफलता तक नहीं ले पहुँचता, तब अनेक बार अधिक समय तक अविचल धैर्य के साथ जुटे रहकर अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करना होता है ।
आतुर मनुष्य इतनी दृढ़ता नहीं रखते, जरा सी कठिनाई या देरी से वे घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं । यही भगोड़ापन उनकी पराजयों का इतिहास बनता जाता है ।
चित्त का एक काम पर न जमना, संशय और संकल्प-विकल्पों में पड़े रहना एक प्रकार का मानसिक रोग है । यदि काम पूरा न हो पाया तो ? यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई तो ? यदि फल उलटा निकला तो ? इस प्रकार की दुविधापूर्ण आशंकाएँ मन को डाँवाडोल बनाए रहती हैं ।
पूरा आकर्षण और विश्वास न रहने के कारण मन उचटा-उचटा सा रहता है । जो काम हाथ में लिया हुआ है, उस पर निष्ठा नहीं होती । इसलिए आधे मन से वह किया जाता है । आधा मन दूसरे काम की खोज में लगा रहता है । इस डाँवाडोल स्थिति में एक भी काम पूरा नहीं हो पाता । हाथ के काम में सफलता नहीं मिलती । बल्कि उलटी भूल होती जाती है, ठोकर पर ठोकर लगती जाती हैं । दूसरी ओर आधे मन से जो नया काम तलाश किया जाता है, उसके हानि-लाभों को भी पूरी तरह नहीं विचारा जा सकता । अधूरी कल्पना के आधार पर नया काम वास्तविक रूप में नहीं, वरन आलंकारिक रूप में दिखाई पड़ता है । पहले काम को छोड़कर नया पकड़ लेने पर फिर उस नए काम की भी वही गति होती है जो पुराने की थी । कुछ समय बाद उसे भी छोड़कर नया ग्रहण करना पड़ता है । इस प्रकार ''काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना'' इस कार्यक्रम की बराबर पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य को अपने असफल जीवन पर पश्चात्ताप करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता ।
मानसिक असंतुलन में आध्यात्मिक पतन मानसिक असंतुलन से केवल सांसारिक और भौतिक क्षेत्र में ही हानि नहीं उठानी पड़ती, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका परिणाम अनिष्टकारी होता है । जो लोग मानसिक उत्तेजना के शीघ्र वशीभूत हो जाते हैं, उनमें अभिमान और लोभ की मात्रा भी बढ़ जाती है और ये दोनों तत्व अन्य अनेक प्रकार के दोषों की उत्पत्ति करते हैं । अभिमान एक प्रकार का नशा है, जिसमें मदहोश होकर मनुष्य अपने को दूसरों से बड़ा और दूसरों को अपने से छोटा समझता है । वह इस बात को पसंद करता है कि दूसरे लोग उसकी खुशामद करें, उसे बड़ा समझें, उसकी बात मानें, जब इसमें कुछ कमी आती है तो वह अपना अपमान समझता है और क्रोध से साँप की तरह फुफकारने लगता है । वह नहीं चाहता कि कोई मुझसे धन में, विद्या में, बल में, प्रतिष्ठा में बज या बराबर का हो, इसलिए जिस किसी को वह थोड़ा सुखी-संपन्न देखता है उसी से ईर्ष्या-द्वेष करने लगता है । अहंकार की पूर्ति के लिए अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहता है । संपन्नता सद्गुणों से, श्रम से, लगातार परिश्रम करने से मिलती है, पर अभिमान के नशे में चूर व्यक्ति सीधे-साधे मार्ग पर चलने में समर्थ नहीं होता, वह अनीति और बेईमानी पर उतर आता है ।
अवमान का अर्थ है-आत्मा की गिरावट । अपने को दीन, तुच्छ, अयोग्य, असमर्थ समझने वाले लोग संसार में दीन-हीन बनकर रहते हैं ।
उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है । कोई साहसिक कार्य उनसे बन नहीं पड़ता । संपन्नता प्राप्त करने और अपने ऊपर होने वाले अन्याय को हटाने के लिए जिस शौर्य की आवश्यकता है, वह अवमानग्रस्त मनुष्य में नहीं होता । फलस्वरूप वह न तो समृद्ध बन पाता है और न अन्याय के चंगुल से छूट पाता है । उसे गरीबी घेरे रहती है और कोई न कोई सताने वाला आए दिन अपनी तीर कमान ताने रहता है । इन कठिनाइयों से बचने के लिए उसे निर्बलतापूर्वक अनीतियों का आश्रय लेना पड़ता है । चोरी, ठगी, कपट, छल, दंभ, असत्य, पाखण्ड, व्यभिचार, खुशामद जैसे दीनता सूचक अपराधों को करना पड़ता है । मोह-ममता, भय-आशंका, चिंता-कातरता, शोक-पश्चात्ताप, निराशा-कुढ़न सरीखे मनोविकार उसे घेरे रहते हैं । आत्मज्ञान एवं आत्मसम्मान को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्योचित मार्ग अपनाना, यह जीवन का सतोगुणी स्वाभाविक क्रम है । यह शृंखला जब विशृंखलित हो जाती है, आत्मिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो पाप करने का सिलसिला चल पड़ता है ।
मानसिक संतुलन और समत्व की भावना मानसिक संतुलन को हम गीता में बतलाई समत्व की भावना भी कह सकते हैं । सब सांसारिक पदार्थों में प्रवृत्ति की हम में जितनी शक्ति होती है, उतनी ही जब उनसे निवृत्त होने की भी शक्ति होती है, तो उस अवस्था को संतुलित और समत्व भावना की अवस्था कह सकते हैं ।
इस समत्व को आचरण में उतारने के लिए केवल विरागी अथवा रागहीन होने से ही कार्य न चलेगा । संतुलित अवस्था तो तब होगी, जब आप रणहीन होने के साथ-साथ द्वेषहीन भी होंगे । हमारे भारतीय साधुओं ने भी वही भूल की । वे होने के लिए तो विरागी हो गए, पर साथ साथ अद्वेषी (अद्वेष्टा) न हुए । राग से बचने की धुन में उन्होंने द्वेष को अपना लिया । संसार के सुख-दुःख से संबद्ध न होने की चाह में उन्होंने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और उसकी सेवाओं से अपना मुख मोड़ लिया ।
जब दो गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवृत्त करते हैं, तो उनके पारस्परिक संयोग से चित्त की जो अवस्था होती है, उसे ही संतुलित अवस्था कहते हैं । दया मनुष्य को दूसरों का दु:ख दूर करने में प्रवृत्त कराती है, पर निर्मोह या निर्ममत्व मनुष्य को दूसरों के सुख-दु:ख से संबंधित होने से पीछे हटाता है। अतएव दया और निर्ममत्व दोनों के एक बराबर होने से चित्त संतुलित होता है । जहाँ दया मनुष्य को अनुरक्त करती है, वहाँ निर्ममता विरक्त । दया में प्रवृत्तात्मक और निर्ममता में निवृत्तात्मक शक्ति है । उसी तरह संतोष और परिश्रमशीलता एकदूसरे को संतुलित करते हैं । परिश्रमशीलता में प्रवृत्तात्मक और संतोष में निवृत्तात्मक शक्ति है । उसी तरह सत्यता और मृदुभाषिता, सरलता और दृढ़ता, विनय और निर्भीकता, नम्रता और तेज, सेवा और अनासक्ति, शुचिता और घृणाहीनता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, तितिक्षा और आत्मरक्षा, निष्कामता और आलस्यहीनता, अपरिग्रह और द्रव्योपार्जन शक्ति परस्पर एकदूसरे को संतुलित करते हैं । इन युग्मों में से यदि केवल एक का ही विकास हो और दूसरे के विकास की ओर ध्यान न दिया जाए तो मनुष्य का व्यक्तित्व असंतुलित एवं एकांगी हो जाएगा । श्रद्धालु व्यक्ति में श्रद्धेय व्यक्ति का अनुगमन करने तथा उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है, स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति पर अंकुश न होने से उसमें निरंकुशता और उच्छृंखलता बढ़ सकती है, दृढ़ प्रकृति व्यक्ति में हठ करने की प्रवृत्ति हो सकती है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति में अभिमान बढ़ सकता है, इत्यादि ।
अतएव जब तक इन व्यक्तियों में क्रमश: आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व, हठहीनता और निरभिमानता का विकास न होगा, तब तक पूर्वोक्त गुण अपनी-अपनी सीमा के भीतर न रहेंगे । अतएव उपरोक्त युग्मों में से प्रत्येक गुण एकदूसरे को मर्यादित करता है और एकदूसरे का पूरक है ।
जब मनुष्य में दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी अपमान सहन करने की क्षमता होती है, जब वह अहिंसा व्रत पालते हुए भी अपराधियों को अधिकाधिक उच्छृंखल, उद्धत, अभिमानी और निष्ठुर नहीं बनने देता, जब वह सेवाव्रती होते हुए भी सेव्यजनों को आलसी, परमुखापेक्षी और अकर्मण्य नहीं होने देता, जब वह क्रोध में होते हुए भी अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना जानता है, जब उसमें भक्ति और उत्साह होते हुए भी दासवृत्ति और उतावलापन नहीं होता, जब वह सफलता में विश्वास रखते हुए भी कार्य करने में लापरवाही नहीं करता, जब वह त्यागी होते हुए भी विपक्षी का लोभ नहीं बढ़ाता, जब वह मान-सम्मान की परवाह न करते हुए भी लोक-कल्याण करने वाले शुभ कार्यों के करने में पूर्ण उत्साही होता है, जब वह अपमान से दुखी न होते हुए भी अपमानजनक कार्य न करने का संयमी एवं आत्मनिग्रही होता है, जब वह शुभ कर्मों को करने के लिए बाध्य न होते हुए भी स्वेच्छा से उन्हें तत्परतापूर्वक अच्छी तरह करता है, जब वह किसी कार्य में प्रवृत्त होने के साथ-साथ उससे निवृत्त भी हो सकता है, तब उसके चरित्र और गुणावलियों में संतुलन आता है ।
जब दो विचारधाराएँ मनुष्य से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य कराती हैं, तब उनके समन्वय से जो स्थिति होती है, उसे संतुलित विचारधारा कहते हैं । आत्मसुख की भावना बहुधा मनुष्य को स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त कराती है और लोकसुख की भावना लोक-कल्याण के कार्यों में । अतएव आत्मसुख और लोकसुख दो विभिन्न दृष्टिकोण हुए । इनके समन्वय से जो स्थिति होती है, वही संतुलित विचारपद्धति है । उसी प्रकार जिसकी विचारधारा में पूर्व और पश्चिम के आदर्शों का समन्वय, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, आदर्श और यथार्थ का समन्वय हुआ है और जो मध्यम मार्ग को अपनाए हुए है, उसी की विचारधारा संतुलित है । जब हम किसी एक ही कार्य के पीछे पड़ जाते हैं अथवा हम जब किसी कार्य में अति करने के कारण दूसरे करणीय कार्यों को भूल जाते हैं, तब हमारी कार्यपद्धति असंतुलित होती है । यदि हम एकदम धन कमाने के पीछे पड़ जाएँ अथवा यदि हम केवल पढ़ने में ही सारा समय बिताने लगें तो हमारी कार्यपद्धति असंतुलित होगी । यदि कोई विद्यार्थी अपने हस्तलेखन की केवल गति ही बढ़ाने पर ध्यान दे और अक्षरों की सुंदरता पर ध्यान न दे तो आप उसके प्रयत्न को क्या कहेंगे ? उसी प्रकार यदि किसी देश में ऐसा कोई आयोजन हो कि केवल शिक्षा की क्वालिटी या उसकी उत्कृष्टता ही एकमात्र लक्ष्य हो और इस बात का ध्यान न हो कि शिक्षा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपलब्ध हो सके तो उस देश के शिक्षाशास्त्रियों की कार्यपद्धति असंतुलित ही कही जाएगी । यही बात मानव जीवन पर भी घटित होती है । हमें केवल एक ही दिशा में घुड़दौड़ नहीं मचानी चाहिए, वरन सब दिशाओं में विकास करते हुए मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए । तभी हम अगाध मानसिक शांति के दर्शन कर सकेंगे ।
'अति सर्वत्र वर्जयेत' हमारे प्राचीन शास्त्रकारों तथा नीतिकारों ने जगह-जगह इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी काम में ''अति'' नहीं करनी चाहिए । यह नियम बुरी बातों पर ही नहीं अनेक अच्छी बातों पर भी लागू होता है ।
जैसे कहा गया है कि अति दानवृत्ति के कारण बलि को पाताल में बँधना पड़ा । संभव है कि कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए जो किसी असाधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं, यह नियम आवश्यक न माना जाए, पर सर्वसाधारण के लिए सदैव मध्यम मार्ग-संतुलित जीवन का नियम ही उचित सिद्ध होता है ।
भगवान बुद्ध ने ''मज्झम मग्ग'' का, मध्यम मार्ग का, आचरण करने के लिए सर्वसाधारण को उपदेश किया है । बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे-धीरे चलने वाले अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचने में पिछड़ जाते हैं । जो मध्यम गति से चलता है, वह बिना थके, बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है ।
पानी में डूब सकता है, किसी दल-दल में फँस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुँह पटक खाकर प्राण गँवा सकता है । साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का कार्य न करे पानी की विस्तृत धारा को देख कर डर जाय तो नदी पार नहीं कर सकता । हाथी बुद्धिमान प्राणी है । वह अपने भारी भरकम डीलडौल का स्थान रखता है नदी पार करने की आवश्यकता अनुभव करता है पानी के विस्तृत फैलाव को समझता है । इन सब बातों का आन रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरता पूर्वक आरम्भ करता है । जहाँ खतरा दीखता है वहाँ से पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह होकर रास्ता ढूँढ़ता है । इस प्रकार वह अपना कार्य पूरा कर लेता है । मनुष्य को भी हाथी की सी बुद्धिमानी सीखनी चाहिए और अपने कार्यों को मध्यम गति से पूरा करना चाहिए । विद्यार्थी कितनी ही उतावली करे एक दो महीने में अपनी शिक्षा पूरी कर नहीं सकता कर भी लेगा तो उसे जल्दी भूल जायगा । क्रम-क्रम से नियतकाल में पूरी हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है । पेड़ पौधे वृक्ष पशु-पक्षी सभी अपनी नियत अवधि में परिपक्व फल देने लायक तथा वृद्ध होते है यदि उस नियति गति विधि में जल्दबाजी की जाय तो परिणाम बुरा होता है । हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता मनोभूमि परिस्थिति आदि को यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूरा करना चाहिए ।
बहुत खाना भूख से ज्यादा खाना बुरा है- इसी प्रकार बिल्कुल न खाना-भूखे रहना बुरा है । अति का भोग मृत है पर अमर्यादित तप भी बुरा है । अधिक विषयी क्षीण हो कर असमय में ही मर जाते है पर जो अमर्यादित अतिशय तप करते है शरीर को अत्यधिक कस डालते हैं वे भी दीर्घ जीवी नहीं होते । अति का कंजूस होना ठीक नहीं पर इतना दानी होना भी किस काम का कि कल खुद को ही दाने-दाने का मुँहताज बनना पड़े । आलस्य में पड़े रहना हानि कारक है पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रह कर जीवनी शक्ति को समाप्त कर डालना भी लाभदायक नहीं । कुबेर बनने की तृष्णा में पागल बन जाना या कंगाली में दिन काटना दोनों ही स्थितियाँ अवांछनीय हैं । नित्य मिठाई ही खाने को मिले तो उससे अरुचि के साथ-साथ दस्त भी शुरू हो जायेंगे । भोजन में मीठे की मात्रा बिल्कुल न हो तो चमड़ी पीली पड़ जायगी । बहुत घी खाने से मन्दाग्नि हो जाती है पैर यदि बिल्कुल घी न मिले तो खून खराब हो जायेगा । बिल्कुल कपड़े न हो तो सर्दी में निमोनिया हो जाने का और गर्मी में लू लग जाने का खतरा है पर, जो कपड़ों के परतों से बेतरह लिपटे रहते हैं उनका शरीर आम की तरह पीला पड़ जाता है । बिल्कुल न पढ़ने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता पर दिन रात पढ़ने की धुन में व्यस्त रहने से दिमाग खराब हो जाता है, आँखें कमजोर पड़ जाती हैं ।
घोर, कट्टर, असहिष्णु, सिद्धान्तवादी बनने से काम नहीं चलता । दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है । अन्य भक्त बनना या अविश्वासी होना दोनों ही बातें बुरी हैं । विवेक पूर्वक हंस की भांति नीर क्षीर का अन्वेषण करते हुए प्राण और अग्राह्य को प्रथक करना ही बुद्धिमानी है । देश काल और पात्र के भेद से नीति व्यवहार और क्रिया पद्यति में भेद करना पड़ता है ।
यदि न करें तो हम अतिवादी कहे जायेंगे । अतिवादी-आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं पर नेतृत्व नहीं कर सकते ।
आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी प्रगति उसी ओर होनी चाहिए, पर सावधान! कहीं अपरिपक्व अवस्था में ऐसी बड़ी छलांग न लगाई जाय जिसके परिणाम स्वरूप टांग टूटने की यातना सहनी पड़े । कड़े कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है । मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवानों का होता है । उतावली करने वाले छछोरे या रेंगने वाले आलसी नहीं महत्त्वपूर्ण सफलतायें वे प्राप्त करते है जो धैर्यवान होते हैं जो विवेक पूर्वक मजबूत कदम उठाते हैं और जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते है ।
नियमितता, दृढ़ता एवं स्थिरता के साथ समगति से कार्य करते रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही उपयोगी संतुलित कार्यों का सम्पादन होता है ।
एकांगी विकास की हानियाँ मानसिक असंतुलन से मनुष्य के व्यक्तित्व का एकांगी विकास होता है । हममें से प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से नई परिस्थितियों में फिट होने का प्रयत्न करता रहता है । यदि हम अपने, घर, पेशे वातावरण के अनुसार अपने मानसिक संस्थान को ढक लेते हैं तो हमें कार्य में प्रसन्नता और मन में शान्ति प्राप्त होती है । अन्यथा हमारा मन अतृप्त और हमारी आत्मा अशान्त रहती है ।
उदाहरण स्वरूप कुछ ऐसे विचार और तथ्य होते हैं जिनके प्रति हम ईर्ष्यालु हो उठते हैं । हम इन विचारों से बच नहीं सकते । उनके बावजूद हमें इन्हीं विरोधी विचारों में कार्य करना है उनसे मित्रता करनी है । तभी हमें मानसिक शान्ति प्राप्त हो उठेगी ।
मन में आन्तरिक संघर्ष का क्या कारण है ? दो विरोधी विचार, दो विभिन्न दृष्टिकोण हमारे मानसिक क्षितिज पर उदित होते हैं । हमें इन दोनों के बाबजूद कार्य करना है । संतुलन ही शान्ति का एक मात्र उपाय है ।
चोरी करने वाला व्यक्ति वह है जो अपने विचार भावना और अन्तरात्मा में पारस्परिक संतुलन नहीं कर पोता । उसकी लालच और मोह की प्रवृत्ति अन्तरात्मा को दबा देती है । वह मोह को लम्बा छोड़ देता है और स्वयं भी उसमें लिपट जाता है । सत्य और न्याय की पुकार दब जाती है । पापमयी वृत्ति की विजय होती है । शैतान बच्चे झगड़ालू औरतें, सब इस मानसिक रोग के शिकार होते हैं । वे मानसिक जगत को ठीक तरीके से संचालित और संतुलित नहीं कर पाते हैं । कोई विकार इतना तीव्र हो जाता है जो विवेक बुद्धि को दबाकर उनके स्वभाव का एक अंग बन जाता है । मन की क्रियाओं को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, १-भावना २-विचार ३-क्रियायें । ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनमें उपरोक्त तीनों क्रियाओं का पूर्ण सामन्जस्य या पूर्ण संतुलन हो । किसी में भावना का अंश अधिक है तो वह भावुकता से भरा है आवेशों को विचार रहता है । उसकी कमजोरी-अति संवेदन शीलता है । वह जरा सी भावना को तिल का ताड़ बनाकर देखता है ।
विचार प्रधान व्यक्ति दर्शन की गुड़ गुत्थियों में ही डूबते उतराते रहते हैं । नाना कल्पनाऐं उनके मानस क्षितिज पर उदित अस्त होती रहतीं है । योजना बनाने का कार्य उनसे खूब करा लीजिए । पर असली काम के नाम वे शून्य हैं ।
तीसरे प्रकार के व्यक्ति सोचते कम हैं भावना में नहीं बहते हैं पर काम खूब करते रहते हैं । इन कार्यों में ऐसे भई काम वे कर डालते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती तथा जिनके बिना भी उनका काम चल सकता है । पूर्ण संतुलित वही व्यक्ति है जिसमें भावना विचार तथा कार्य इन तीनों ही तत्वों का पूर्ण सामंजस्य या मेल हो । ऐसा व्यक्ति मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ है । हमें चाहिए कि हम अति से अपनी रक्षा करें और इस प्रकार असंतुलन से बचे रहे । कहने का तात्पर्य यह है कि अति भावुकता के चक्र में पड़ कर ऐसा न कर डाले ऐसे वायदे न कर बैठें जिन्हें बाद में पूर्ण न कर सकें । इतने विचार-प्रधान न बन जायें कि सम्पूर्ण समय सोचते विचारते चिन्तन करते-करते ही व्यतीत हो जाय । विचार करना उचित हैं किन्तु विचारों ही में निरन्तर डूबे रहना और कार्य न करना हमें मानसिक रूप से आलसी बना डालेगा ।
अच्छे व्यक्ति के निर्माण में क्रिया भावना, तथा विचार शक्ति इन तीनों आवश्यक तत्वों का पूर्ण विकास होना चाहिए । जो व्यक्ति काम क्रोध आवेश उद्वेग इत्यादि में निरत रहते हैं उन्हें भावनाजन्य मानसिक व्याधियों का परित्याग करना चाहिए । जो केबल कागजी योजना से और व्योम-विहारिणी कल्पनाओं में लगे रहते हैं, इन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से अपनी योजनाओं की सत्यता जांचनी चाहिए । इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अपने कार्यों को जीवन में प्रकट करना चाहिए । हम महान पुरुषों में देखते हैं कि उनकी बुद्धि पूर्ण विकास को पहुँच चुकी थी, विचार और इच्छा शक्ति बड़ी बलवती थी और कार्य शक्ति उच्चकोटि की थी । महात्मा गाँधी ऐसे संतुलित व्यक्तित्व के उदाहरण थे ।
जीवन में संतुलन का महत्त्व एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हवा के भयंकर तूफान में चला जा रहा है । धूल से उसके नेत्र क्षण भर के लिए बन्द हो जाते हैं । अधिमिचे नेत्रों से वह दूसरी ओर बहक जाता है । ठीक मार्ग पर आरुढ़ होना चाहता है किन्तु मार्ग नहीं सूझता ।
यही हाल मानव के अन्तर्जगत का है । वह अन्दर ही अन्दर अनेक विरुद्ध भावनाओं का शिकार रहता है । प्रलोभन का मायाजाल और वासना की आँधी उसे घेरे रहती है और वासना तृप्ति के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है । उसे पथ भ्रष्ठ होते देख उसकी शुभ शक्तियां उसे सचेत करती हैं । यदि उनकी शक्ति अधिक हो तो व्यक्ति बच जाता हैं, अन्यथा पतन के गर्त में विलीन हो जाता हैं ।
मानव जीवन में अनेक आन्तिरिक एवं बाह्य शक्तियों का प्राधान्य है । भावना कहती है-
''अमुक व्यक्ति बड़ी दयनीय स्थिति में है । उसकी सहायता करें, अपने सुख सुविधा, साधनों को न देखें । कर्ण, शिवि, राजा हरिश्चन्द्र का उदाहरण लीजिए । इन महापुरुषों ने दया करुणा सहानुभूति और दान द्वारा महान पद प्राप्त किया । हमें भी यही करना चाहिए । अपने सुख सुविधा इत्यादि का कोई आन न रखना चाहिए ।'' तर्क आपको रोकता है और कहता है- ''क्या पागल हुए हो सोचो विचारों दिमाग से काम लो । यदि साधनों का ध्यान छोड़कर व्यय किया दूसरों से बड़े बड़े वायदे किए तो आफत में फँस जाओगे । भावना में मत बहो । समाज रुपये का आदर करता है ।'' विलास भावनाऐं कहती हैं- "अरे मानव तूने बहुत श्रम कर" लिया है । अब कुछ आनन्द मना ले । जीवन का रस ले । बार-बार जीवन आने वाला नहीं है ।"
इस प्रकार मानव के आन्तरिक जीवन में भावना तर्क वासना शरीर बल, आत्म बल, प्रेम द्वेष, घृणा इत्यादि परस्पर विरुद्ध शक्तियों का अविराम ताण्डव चलता रहता है । जो इन शक्तियों का उचित समन्वय कर सकता है वही सफल है । जीवन में भावना की आवश्यकता है बिना भावना का मनुष्य मिट्टी या पत्थर का पुतला मात्र बन जाता है । तर्क अर्थात् विवेक की आवश्यकता भी है । जो सोच समझ कर कार्य न करे, बुद्धि से काम न ले वह तो निराट पशु ही है । इसी प्रकार वासना, घृणा, प्रेम इत्यादि सबका अपने अपने स्थान पर महत्त्व है । पर सुख और सफलता मानव की विभिन्न शक्तियों के संतुलन में ही है । असंतुलन में पराजय छिपी हुई है ।
सिकन्दर महान, जूलियस सीजर और औरंगजेब की अत्यंत बड़ी महत्त्वाकांक्षाओं का परिणाम हमारे सामने है । कर्ण के पतन का कारण अति भावुकता थी, रावण दर्प के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ । तर्कशील, भावनाशील, कर्मशील-तीनों ही प्रकार के मानव जीवन में अमर्यादित संतुलन से असफल हो सकते हैं । इसलिए यह ध्यान रखें कि कहीं आपके व्यक्तित्व का एक ही पहलू विकसित न होता रहे । सभी संतुलित रूप में विकसित होते रहें । अतिरेक त्याज्य है । ध्येय और व्यवहार कर्म और भावना, परिश्रम और विश्राम तर्क और कार्य इन सभी द्वन्द्वों में उचित समन्वय का नाम ही जीवन है ।