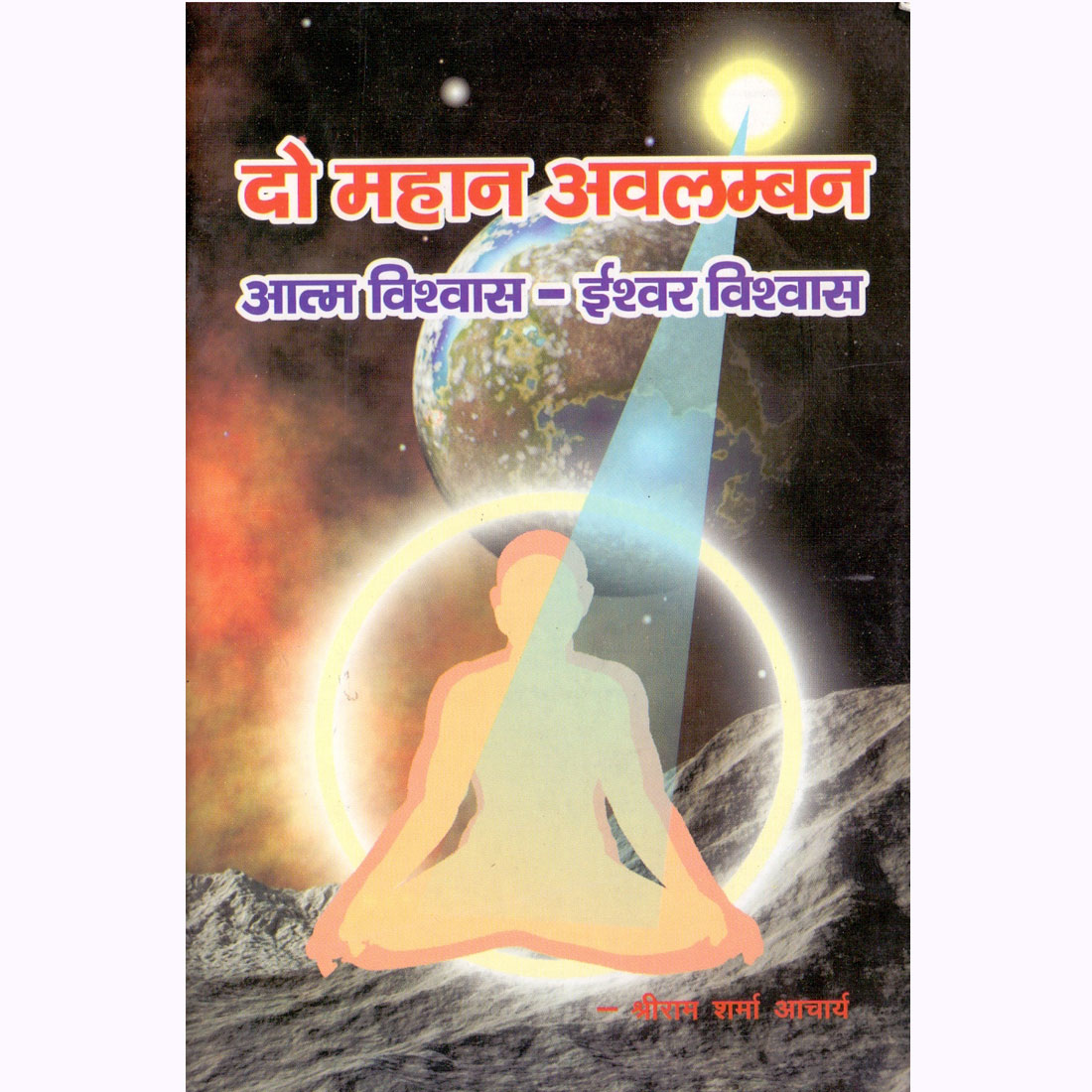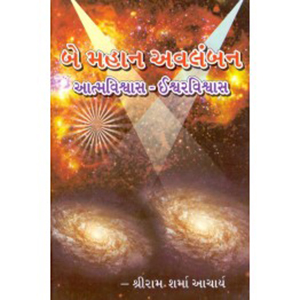दो महान अवलम्बन 
मनुष्य महान है और उससे भी महान है उसका भगवान
Read Scan Versionसच कहा जाय तो इस संसार में दो वस्तु बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा परमेश्वर और एक हम स्वयं। इन दो से बढ़कर और कुछ आश्चर्यजनक और सामर्थ्य सम्पन्न तत्व इस दुनिया में हमारे लिए हो ही नहीं सकते। यदि अपनी महिमा, और क्षमता को समझ लिया जाय और उसका बुद्धिमत्ता एवं व्यवस्था के साथ उपयोग किया जाय तो उसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि संसार के साथ ही हम स्वयं उसे देखकर दंग रह जाएं। मनुष्य देखने में जितना तुच्छ और हेय लगता है वस्तुतः वैसा है नहीं। उसकी सम्भावनायें अनन्त हैं। गड़बड़ इतनी भर पड़ जाती है कि वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता और जितना कुछ समझा है उसका सदुपयोग करने के लिए जो प्रचलित ढर्रा बदलना चाहिए उसके लिए मनोबल और भावनात्मक साहस एकत्रित नहीं कर पाता। यदि इस छोटी-सी त्रुटि को संभाल सुधार लिया जाय तो उसके अद्भुत विकास की सारी सम्भावनायें खुल जाती हैं। जिस भी दिशा में उसे बढ़ना हो—उस पथ के समस्त अवरोध स्वयमेव हट जाते हैं।
देवताओं की चर्चा कही-सुनी बहुत जाती है पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। यदि दर्शन करने हों तो अपने परिष्कृत स्वरूप में अपने आप का दर्शन करना चाहिए। इस छोटे से कलेवर में समस्त देव शक्तियां एक ही स्थान पर केन्द्रीभूत मिल सकती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में भूः भुवः स्वः पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक सन्निहित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तीनों शक्तियां इसी में भरी पड़ी हैं। दसों इन्द्रियों में दस दिग्पाल बसते हैं। मनुष्य जीवन एक समुद्र है जिसके आस-पास शेष सर्प, सुमेरु पर्वत, देव, असुर और कच्छप भगवान चिरकाल से विराजमान हैं और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आत्मबल का धनी उनका सदुपयोग करे और इस समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र मन्थन की पौराणिक कथा पुरानी हो गई। इस कथानक की पुनरावृत्ति हममें से कोई भी कर सकता है, यदि जीवन संघर्ष और जीवन के सदुपयोग की विधि व्यवस्था और पद्धति समझ में आ जाये। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, हमारे लिए सिद्धियां और विभूतियां 1400 उपहार लेकर सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। सचमुच हम स्वयं एक आश्चर्य हैं काश, हमने अपने को समझ पाया होता। और उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है? इसका विनियोग समझ पाया होता तो इन परिस्थितियों में कदापि न पड़े होते जिनमें आज पढ़े हुए हैं।
अपने आपे से भी बड़ा आश्चर्य है अपना भगवान। उसके एक विनोद कल्लोल भर का प्रयोजन पूरा करने के लिए यह इतना बड़ा विश्व बनकर खड़ा हो गया है, जिसकी विशालता की कल्पना तक कर सकना कठिन है। वह अकेला था, उसकी इच्छा अपना विस्तार देखने की—अपने आप में रमण करने की हुई सो इस इच्छा मात्र ने इतने विशाल विश्व का सृजन खड़ा कर दिया। यह तो उसकी इच्छा का चमत्कार हुआ। उसकी सामर्थ्य और क्रिया का परिचय तो प्राप्त करना अभी शेष ही रह गया। मनुष्य मुद्दतों से प्रकृति के रहस्य जानने और उसकी ईथर, विद्युत, आणविक आदि शक्तियों के उपयोग का मर्म समझने के लिए चिरकाल से प्रयत्न कर रहा है। इस पुरुषार्थ से उसे कुछ मिला भी है। उसका परिणाम इतना ही है कि छोटा बच्चा इस गुब्बारे को पाकर उछल-कूद ही सके। पर प्रकृति के जितने रहस्य अभी जानने को शेष हैं उसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियां उतनी कम हैं जितना कि पर्वत की तुलना में धूलि का एक कण। भगवान की अगणित कृतियों से अति तुच्छ सी कृति अपनी धरती का वैभव इतना विशाल है कि मनुष्य की तृष्णा इच्छा और कल्पना से असंख्य गुना वैभव उसमें भरा पड़ा हैं। फिर समस्त ब्रह्माण्डों से मिलकर बने हुए इस महान सृजन में भरी विभूतियों की बात सोची ही कैसे जाय?
इतने विशाल वैभव से भरे हुए विश्व को एक विनोद उल्लास की तरह बनाने और चलाने वाला परमेश्वर यदि समग्र रूप से मनुष्य की कल्पना में आ सका होता तो कितना सुखद होता। पर कहां मनुष्य कहां उसकी कल्पना! इनकी तुच्छता और भगवान की विशालता की आपस में कोई संगति नहीं बैठती। उसका समग्र स्वरूप तो सत्चित् आनन्द से सत्यं शिव सुन्दरम् से इतना ओत-प्रोत है कि उसकी एक बूंद पाकर भी मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है।
निस्सन्देह हमारा आपा महान है और निश्चय ही हमारा परमेश्वर अत्यन्त ही महान है। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा आश्चर्य और शेष रह जाता है वह है इन दोनों के मिलन से उत्पन्न होने वाली वह धारा जिसमें सन्तोष और शान्ति की—आनन्द और उल्लास की—सुख और साधनों की असीम तरंगें निरन्तर उद्भूत होती रहती है। यों जब भी दो श्रेष्ठताएं मिलती हैं तब उनके सुखद परिणाम ही होते हैं। ऋण और धन विद्युत धाराएं मिलकर रोमांचकारी शक्ति प्रवाह में परिणत हो जाती हैं और उनके द्वारा अनोखे काम सम्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष का मिलन न केवल हृदय की—कली को खिला देता है वरन् एक नये परिवार—नये समाज, का सृजन ही आरम्भ कर देता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना सुखद कितना सक्षम और कितना अद्भुत हो सकता है, इसकी कल्पना भी कर सकना यदि हमारे लिए सम्भव हो रहा होता तो तृष्णा वासना की जिस फूहड़ परितृप्ति के लिए मृग मरीचिका में भटकते फिर रहे हैं उसे छोड़ कर अपनी गतिविधियां उस दिशा में बदलते जिसमें उस परम मिलन से उत्पन्न होने वाली अजस्र शान्ति और शक्ति की सम्भावना प्रत्यक्ष प्रस्तुत होती है।
आत्मा और परमात्मा की दो परम सत्ताओं के परस्पर मिलन के प्रयत्न को ही ‘योग’ कहते हैं। ‘योग’ शब्द का अर्थ ही जोड़ना या मिलन है। किसका जोड़—किससे जोड़—इसका एक ही उत्तर है आत्मा से परमात्मा का मिलन। यह प्रक्रिया सम्पन्न की जा सके तो उसके परिणाम और फलितार्थ भी उतने ही अद्भुत हो सकते हैं जितने कि ये दोनों तत्व स्वयं में अद्भुत हैं। बूंद समुद्र में मिल जाय तो वह खोती कुछ नहीं अपनी व्यापकता बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना मूल्य ही बढ़ा लेता है। लोहा पारस को छूकर घाटे में थोड़े ही रहता है। यह स्पर्श उसके सम्मान की वृद्धि ही करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन निस्सन्देह आत्मा के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, पर इसके योगदान से परमात्मा भी कम प्रसन्न नहीं होता। इस व्यक्त विश्व में उसकी—अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है, जो हो रहा है वह परदे के पीछे अदृश्य ही तो है। उसे मूर्तिमान दृश्य बनाने के लिए ही तो यह विश्व सृजा गया था। जड़ पदार्थों से वह प्रयोजन पूरा कहां होता है। चैतन्य जीवधारी के बिना इस धरती का समस्त वैभव सूना अनजाना ही पड़ा रहेगा। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग सम्भव हो, और उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकती है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतीक प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता, जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया था। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की। बहुत बने तो जरूर पर यदि उसके अनुरूप, उस जैसे न हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहां पूरा हुआ? आनन्द तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है। बन्दर और सूअर का साथ कहां जगेगा? आदमी की शादी कुतिया से कैसे होगी? पानी में लोहा कैसे घुलेगा? बच्चों का खेल बच्चों में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है, हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। कसाई और पण्डित की दिशा अलग है। मनुष्यों में ऐसे भी कम नहीं हैं जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिलकुल विमुख होकर चलते हैं। असुरता को पसन्द और वरण करने वाले लोगों की कमी कहां है? सच पूछा जाय तो माया ने सभी की बुद्धि को तमसाच्छन्न बनाकर अज्ञानान्धकार में भटका दिया है और वे सुख की तलाश आत्म तत्व में करने की अपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहां उसके मिलन की कोई सम्भावना नहीं है। मृग तृष्णा में भटकने का दोष बेचारे नासमझ हिरन पर ही लगाया जाता है। वस्तुतः हम सब समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं और आत्मानुभूतियों का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने—बालू में तेल निकालने जैसी विडम्बनाओं में उलझे पड़े हैं। जिस उपहासास्पद स्थिति में हमारा चेतन उलझ गया है उसमें न उसे सुख मिलता है न शान्ति ही, उलटी शोक-सन्ताप भरी उलझनें ही सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती हैं।
इन परिस्थितियों में उलझे हुए ईश्वर की अभीप्सित दिशा में चलने और उसके विनोद में सहचर बनने वाले व्यक्ति बनते ही कहां हैं? अन्धी भेड़ों की तरह हम सब तो शैतान के बाड़े में जा धंसे। ईश्वर का विनोद प्रयोजन पूरा कहां हुआ? उसे साथी सहचर कहां मिले? सृष्टि बनी तो सही—जड़ चेतन भी उपजे पर भगवान का खेल जिसमें विनोद और उल्लास का निर्झर निरन्तर झरना चाहिए था अवरुद्ध और शुष्क ही रह गया। शैतान ने भगवान का खेल ही बिगाड़ दिया। यों यह भी एक खेल है पर वैसा नहीं जैसा कि चाहा गया था। इस व्यवधान को हटा सकने में समर्थ जो आत्माएं परमात्मा की विनोद मण्डली में सम्मिलित हो जाती हैं वे उसकी प्रसन्नता का कारण भी बनती हैं। अपने को जो परमेश्वर के समीप ले पहुंचते हैं, इस विश्व को अधिक सुन्दर बनाने के भगवत् प्रयोजन में साथी बनते हैं, निस्सन्देह वे परमात्मा की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसके इस संसार की गरिमा को प्रखर बनाते हैं। ऐसी आत्माओं का मिलन परमात्मा को भी प्रिय एवं सन्तोषजनक ही लगता है।
भक्त भगवान को तलाशता है और भगवान भक्त को ढूंढ़ते हैं। कैसी आंख मिचौनी है कि कोई किसी को मिल नहीं पाता। तथाकथित भक्तों की कमी नहीं। वे तलाशते भी हैं पर मिल नहीं पाते। इसलिए कि उन्हें न तो भगवान का स्वरूप मालूम है, न प्रयोजन, न मिलने का मार्ग। खुशामद और रिश्वत मनुष्यों को आकर्षित करने वाला फूहड़ तरीका ही लोगों के अभ्यास में रहता, है सो वे उसे भी भगवान पर प्रयुक्त करते हैं। लम्बी चौड़ी शब्दावली का उच्चारण करके भगवान को इस प्रकार बहकाने का प्रयत्न करते हैं मानो वह उच्चारण को ही यथार्थ समझता हो और मानो अन्तरंग की स्थिति का उसे पता ही न हो। स्तोत्र पाठ और कीर्तनों की बवण्डर हमें सुनाई पड़ती है यदि उसके मूल में मिलन की भावना भी सन्निहित रही होती तो कितना अच्छा होता। पर मिलन का तो अर्थ ही नहीं समझा जा सका। मिलन का अर्थ होता है समर्पण—समर्पण का अर्थ है विलीन होना। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो अपना स्वरूप, स्वभाव सभी खो देती है और समुद्र की तरह ही लहराने लगती है। चूंकि समुद्र खारा है इसलिए बूंद अपने में भी खारापन ही भर लेती है कोई ऐसा चिन्ह शेष नहीं रहने देती, जिससे उसका अस्तित्व अलग से पहचाना जा सके। ईश्वर से मिलन का अर्थ है अपने आप को गुण, कर्म स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर जैसा बना लेना और अपनी आकांक्षाओं तथा गतिविधियों को वैसा बना लेना जैसा कि ईश्वर की हैं अथवा उसे हमसे अभीष्ट है। मिलन का इतना दायरा जो समझ सकता है। उसी की चेष्टायें तदनुरूप हो सकती हैं। जिसने वस्तु स्थिति को समझा नहीं, वह चापलूसी का—खुशामदखोरी का धन्धा अपनाकर वैसे ही ईश्वर को भी अपने वाक् जाल में बांधना चाहता है जैसे कि अहंकारी और मूर्ख लोगों को चापलूस अपने जाल में फंसा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
दूसरा तरीका ओछे लोगों को कुछ प्रलोभन या रिश्वत देकर किसी को अपने पक्ष में करने का रहता है। वे इस हथियार से ही लोगों से अपना मतलब निकालते हैं, थोड़ी रिश्वत देकर फायदा उठाने की कला उन्हें मालूम रहती है। ऐसे ही ईश्वर को भी थोड़ा प्रसाद, वस्त्र, छत्र, मन्दिर आदि के प्रलोभन देकर उससे अपनी भौतिक आकांक्षायें पूरा करा लेने की बात लगाते रहते हैं। वे याचनायें उनके पुरुषार्थ के अनुरूप हैं या नहीं, उन्हें संभालने सदुपयोग कर सकने की क्षमता भी है या नहीं, वे नीति न्याय एवं औचित्य युक्त भी हैं या नहीं, इतना सोचने की किसे फुरसत है? ईश्वर हमारी कामनायें पूरी करे और बदले में थोड़ा उपहार रिश्वत के रूप में दे दें। इतनी ही बुद्धि इन तथाकथित भक्तों की काम करती है और वे शब्दाडम्बर तथा उपहार प्रलोभन के तुच्छ आधारों से ऊंची बात सोच ही नहीं पाते। फलस्वरूप उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। इन तथाकथित भक्तों में से किसी को भी भगवान नहीं मिलता और उनके सारे क्रिया-कृत्य निष्फल चले जाते हैं।
भगवान को भी भक्त नहीं मिलते और उसे भी इस उपलब्धि के आनन्द से वंचित रहना पड़ता है। माता बच्चे को गोद में तब उठाती है जब उसकी टट्टी से सनी हुई देह की सफाई हो जाती है। बच्चा भले ही रोता रहे पर जब तक वह गन्दगी से सना है गोदी में नहीं उठाया जाएगा। उसे माता की निष्ठुरता कहा जाय—कहते रहें पर बात तो उसी तरह बनेगी जो उचित है। सफाई आवश्यक है। उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मनुष्य को अपने कषाय-कल्मषों की मलीनता धोनी ही पड़ेगी। अन्तःकरण को निर्मल और निश्चल बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना उसकी गणना उन भक्तों में न हो सकेगी जो प्रभु से मिलन का लाभ उठा सकने के अधिकारी होते हैं।
दूसरा कदम है ईश्वर की इच्छानुसार अपने को ढाल लेने का साहस। पतिव्रता स्त्री अपने स्वभाव आचरण एवं क्रिया कलाप को पति की इच्छानुरूप ढाल लेती है। इसके बिना दाम्पत्य जीवन कैसा? मिलन का आनन्द कहां? समर्पण के आधार पर ही अद्वैत के रूप में परिणित हुआ जाता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर—उसके संकेत और निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा और क्रिया में जोड़ देना, इसी का नाम समर्पण है, मिलन की साधना इसी से पूरी होती है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना और नाक रगड़ना, भला यह भी कोई भक्ति है। लोभ और मोह की पूर्ति के लिए दांत निपोरना भला यह भी कोई प्रार्थना है। इस प्रकार की भक्ति को वेश्यावृत्ति ही कहा जा सकता है। भौतिक स्वार्थ के लिए किए गए क्रिया-कलापों को ईश्वर के दरबार में भक्ति संज्ञा में नहीं गिना जा सकता। वहां तो भक्त की कसौटी यह है कि किसने अपनी कामनाओं और वासनाओं को तिलांजलि देकर ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया और उसकी मर्जी के अनुरूप चलने के लिए कठपुतली की तरह कौन तैयार हो गया? जो इस कसौटी पर खरा उतरता है—वही भक्त है। भक्त भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने के लिए विवश नहीं करता, वरन् उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिलाकर अपनी विचार प्रणाली एवं कार्य-पद्धति का पुनर्निर्माण करता है। तब उसके सामने इस विश्व को अधिक सुन्दर, अधिक समुन्नत और अधिक श्रेष्ठ बनाने की ही एकमात्र इच्छा शेष रह जाती है। अपने आपको काया की तथा परिवार की तुच्छता में आबद्ध नहीं करता वरन् सबमें अपनी आत्मा को—और अपनी आत्मा में सबको समाया हुआ समझ कर लोक-मंगल के लिए जीता है और वसुधैव कुटुम्बकम् के अनुरूप अपनेपन की परिधि अति व्यापक बना लेता है। तब उसे अपनी काया ईश्वर के देव मंदिर जैसी दीखती है और अपनी सम्पदा ईश्वर की पवित्र अमानत जैसी, जिसका उपयोग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए किया जाता है।
इन मान्यताओं को अन्त:करण में गहन श्रद्धा की तरह प्रतिष्ठापित कर लेने वाला व्यक्ति भक्त है। उसे ईश्वर दर्शन के रूप में किसी अवतार या देवता की काल्पनिक छवि को आंख से दीख पड़ने की बात—बुद्धि उठाती ही नहीं। वह उसे दिवास्वप्न मात्र मानता और निरर्थक समझता है। उसका ईश्वर दर्शन अधिक वास्तविक और बुद्धि संगत होता है। जो अपनी विचारणा और प्रक्रिया में ईश्वर की प्रेरणा को चरितार्थ होते देखता है जिसकी आत्मा में ईश्वर के सत्पथ पर चलने की पुकार सुनाई पड़ती है, समझना चाहिए उसमें ईश्वर बोलता है—बात करता है—साथ रहता है और अपनी गोदी में उठाने का उपक्रम करता है। भक्ति की सार्थकता इसी स्थिति में है।
अपनी महानता में विश्वास रखें—
जिनमें ऊंचे दर्जे की आत्म-श्रद्धा थी वे अपने आरम्भ किए कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में अडिग विश्वास रखते थे। ऐसे ही स्त्री-पुरुषों ने मानव-संस्कृति में चमत्कार करके दिखाए हैं।
कितने ही मनुष्यों में जिस वस्तु के ऊपर श्रद्धा थी, अन्य लोगों ने उसे काल्पनिक अथवा तुच्छ बतलाया था। पर वे उस कार्य को सिद्ध करने में—उस वस्तु को मूर्त रूप देने में अपूर्व सहन-शक्ति का परिचय देते हुए निरन्तर संलग्न रहे। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य जाति को ऐसे साधन प्राप्त करा सके कि जिनसे प्रगति में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। यदि वे ऐसा न करते तो आज हम कई शताब्दी पुरानी अवस्था में ही पड़े दिखाई देते।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सफलता की आशा रखे बिना, अभिलाषा किए बिना, उसके लिए दृढ़ प्रयत्न किए बिना ही सफलता प्राप्त कर सको। प्रत्येक ऊंची सफलता के लिए पहले मजबूत, दृढ़ आत्म-श्रद्धा का होना अनिवार्य है। इसके बिना सफलता कभी मिल नहीं सकती। भगवान के इस नियमबद्ध और श्रेष्ठ व्यवस्था युक्त जगत में ‘दैव-योग’ के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य नहीं पूर्ण कारण होना चाहिए, परिणाम जितना बड़ा हो कारण भी उसी के मुकाबले में होना आवश्यक है। नदी का पानी कभी उसके मूल निकास स्थान की अपेक्षा ऊंचा नहीं चढ़ सकता। महान सफलता प्राप्त करनी हो तो महान आत्म श्रद्धा भी रखनी चाहिए, और उसी प्रकार संलग्नतापूर्वक कार्य करना चाहिए। आपकी शक्ति चाहे जैसी बड़ी हो, तो भी आप अपने कार्य में उतनी ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे जितनी कि आपकी आत्म-श्रद्धा होगी। जो मनुष्य कार्य सिद्धि करने की श्रद्धा रखता है वही कार्य को पूरा कर सकता है। और जिसमें ऐसा विश्वास नहीं है वह कार्य को सिद्धि नहीं कर सकता। यह एक पक्का और निर्विवाद नियम है।
आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मत्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहें तो उसकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रहो। अगर उसकी आत्म-श्रद्धा को खो देते हो तो तुम्हारे अपने व्यक्तित्व को हार माननी पड़ेगी।
किसी मनुष्य के कहने से अथवा किसी आपत्ति के आने से पहले आत्म विश्वास को डगमगाने मत दो। कदाचित् आप अपनी सम्पत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश और अन्य लोगों के सम्मान को खो बैठो, पर जब तक आप अपने ऊपर श्रद्धा कायम रखोगे तब तक आपके लिए आशा है। यदि आत्म-श्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी ही या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही।
एक अवसर पर एक फौजी सिपाही नैपोलियन के पास इतनी शीघ्रता से एक सन्देश लाया कि उसने पत्र दिया उससे पहले ही उसका घोड़ा मरकर गिर गया। नैपोलियन ने तुरन्त उस सन्देश का उत्तर लिखाया और सिपाही से कहा कि अब मेरे घोड़े पर बैठकर जितनी जल्दी हो सके इस उत्तर को अपने अफसर के पास पहुंचाओ।’’
उस सिपाही ने उससे बढ़िया साज वाले दर्शनीय प्राणी की तरफ देखा और कहा—‘‘सेनापति साहब! एक साधारण सिपाही के लिए ऐसा सुशोभित और भव्य घोड़ा शोभा नहीं दे सकता।’’
नैपोलियन ने कहा—‘‘एक फ्रांसीसी सैनिक के लिए कितनी भी श्रेष्ठ और कैसी भी भव्य वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है।’’
इस गरीब फ्रांसीसी सैनिक की तरह संसार के अधिकांश मनुष्य यह मानते रहे हैं, कि भाग्य देवता के लाड़ले पुत्रों को जो दर्शनीय और उत्तम पदार्थ मिले हुए हैं, हम उनके अधिकारी नहीं हो सकते। अपने व्यक्तित्व को छोटा समझने अथवा अपने को हीन समझने की यह मनोवृत्ति उनको ऐसा निर्बल बनाती है कि इससे वे अपने व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा नहीं रखते, उस से पूरी आशा नहीं करते, पूरी मांग उपस्थित नहीं करते।
अगर तुम एक बौना का ही अभिनय करते रहे तो तुम भीमसेन कभी नहीं बन सकते। प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पर बौनापन का विचार करते रहने से भीमसेन की उत्पत्ति हो सके। जैसा आदर्श होता है वैसी ही प्रतिभा भी बनती है। मन में जैसा बनने का विचार होता है, वही मनुष्य का आदर्श होता है।
बहुत से लोगों को आरम्भ से यही सिखाया गया है कि संसार की उत्तमोत्तम वस्तुएं उनके लिए नहीं पैदा की गई हैं। इसलिए उन लोगों के दिमाग में बचपन से ही यह बात बैठ गई है कि वे घटिया श्रेणी के हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक स्त्री-पुरुष जो बड़े काम कर सकने की शक्ति रखते हैं छोटे-छोटे मामूली कामों में ही जीवन बिता देते हैं। ये अपने व्यक्तित्व से न तो पूरी आशा रखते हैं और न हृदय से उतना उद्योग करते हैं। हीनत्व की भावना के फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व शक्ति होते हुए भी दबा हुआ रह जाता है।
हम लोग अपने महान् जन्मसिद्ध अधिकार को पूरी तरह नहीं समझ पाते, और हम कितनी उन्नति करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, कितने अंशों में हम अपने स्वामी बन सकते हैं, इस बात को भी नहीं जानते। अगर हम लोग चाहें तो अपने भाग्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जो-जो कार्य अन्य लोगों के लिए सम्भव है उनको हम भी कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं, यह बात भी अभी हमारी समझ में नहीं आई है।
प्रसिद्ध विदुषी मेरी करेली ने लिखा है कि ‘‘अगर हम मिट्टी के ढेले से अधिक उच्च बनने की इच्छा न रखते हों तो हम वास्तव में मिट्टी के ढेले ही बन जायेंगे और अधिक वीर तथा योग्य लोग हमारे ऊपर होकर निकल जायेंगे।’’
अगर आप यही विचार किया करोगे कि आप दूसरों के समान श्रेष्ठ नहीं हो, वरन् निर्बल तथा सत्वहीन प्राणी हो, तो आपका जीवन स्तर वास्तव में घटिया हो जाएगा और आपकी शक्ति कुंठित हो जाएगी।
हम जो कार्य करना चाहते हैं उसे श्रद्धापूर्वक आरम्भ करने से, श्रेष्ठ रीति से करते रहने से ही अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अगर आप महान् कार्य करने की आकांक्षा रखते हों तो आपको विशाल कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए और तदनुसार उत्तम कार्य करना चाहिए।
जो मनुष्य अपने व्यक्तित्व की अधिक और ठीक कीमत आंकता है और अपनी सफलता के विषय में विश्वास रखता है, उसमें कोई ऐसा तत्व होता है कि चोट करने के पहले ही वह आधी लड़ाई जीत लेता है। अपने को घटिया और शून्यवत् समझने वाले लोगों के सामने प्रायः जो बाधायें आया करती हैं वे उसके मार्ग से हट जाती हैं।
हम अनेक बार किसी व्यक्ति के बारे में यह सुना करते हैं कि ‘‘यह मनुष्य जिस कार्य को हाथ में लेता है उसे पूर्ण कर लेता है, वह जिस वस्तु को स्पर्श करता है वह स्वर्ण बन जाती है।’’ ऐसा मनुष्य अपने चरित्र-बल और बुद्धिमत्ता से अत्यन्त प्रतिकूल संयोगों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही श्रद्धा को उत्पन्न करती है और बल प्रदान करती है।
जो मनुष्य विजय प्राप्त करने वाला होता है वह चारों तरफ विश्वास का प्रसार करता है, और जिस काम को उसने उठाया है उसको पूर्ण करने की शक्ति उसमें है, ऐसी श्रद्धा अन्य लोगों में भी उत्पन्न कर देता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उसे अपनी विचार शक्ति का ही नहीं, वरन् अपने से परिचय रखने वालों की विचार शक्ति का भी सहारा मिलता है। उसके मित्र तथा परिचित व्यक्ति बारम्बार यह कहकर कि ‘वह सफलता प्राप्त करने में समर्थ हैं’ उसे विजयी बनाने में सहायक होते हैं। उसे जितनी सफलतायें मिलती जाती हैं, उसकी गम्भीरता, विश्वास, श्रद्धा, शक्ति में वैसे-वैसे ही वृद्धि होती जाती है। जैसे अमेरिका के प्राचीन रेड-इण्डियन जाति वाले यह समझा करते थे कि वे जितने शत्रुओं को जीतते जाते हैं, उतनी ही उनकी शक्ति उनको प्राप्त होती जाती है, उसी प्रकार वास्तव में युद्ध, उद्योग, व्यापार, आविष्कार, विज्ञान अथवा कला प्राप्त होने वाली प्रत्येक विजय विजेता की शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाती जाती है।
जिस कार्य को सिद्ध करने की आपकी इच्छा हो उसको इतनी दृढ़ता, इतने निश्चय और इतने मजबूत संकल्प के साथ हाथ में लो कि जब तक वह पूरा न हो तब तक कोई उसे तुम्हारे हाथ से छीन न सके।
श्रद्धा ही हमारी मानसिक सेना का नैपोलियन है। वह अन्य सब शक्तियों को दुगुना-तिगुना बलवान बना देती है। जब श्रद्धा नेता बनी रहती है तब तक समस्त मानसिक सेना ठहरी रहती है। घुड़-दौड़ का घोड़ा भी एक बार आत्म-श्रद्धा गंवा देने के पश्चात् इनाम नहीं जीत सकता। आत्मश्रद्धा में से उत्पन्न होने वाली हिम्मत हमारे भीतर संचित बल के अन्तिम से अन्तिम अंश को भी बाहर खींच लाती है।
अनेक व्यक्ति जो असफल होते हैं उसका कारण यह है कि वे विजय के लिए हर तरह का त्याग करने का निश्चय करके कार्यारम्भ नहीं करते। कभी पीछे की तरफ दृष्टिपात न करने वाली आत्म-श्रद्धा उनमें नहीं होती। किसी कार्य को केवल सामान्य भावना से करते रहना और उसमें अपनी समग्र शक्ति को उपयोग करना, अपनी समस्त कर्तव्य शक्ति को उसमें झोंक देना, इन दोनों के बीच काफी अन्तर रहता है। साधारण कार्य और महान् उद्देश्य लेकर कार्यारम्भ करने में यही अन्तर है।
अपने व्यक्तित्व के विषय में आप स्वयं जो विचार रखते हैं, उसी से आपकी शक्तियों का ठीक-ठीक पता लग सकता है। अगर आपकी बुद्धि विशाल नहीं है, यदि आप में साहस कर सकने का गुण नहीं है, यदि दृढ़ आत्मश्रद्धा नहीं है, तो आप कभी महत्कार्य नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा का तात्पर्य मनुष्य के उच्च आदर्श और उन्नत उद्देश्यों से होता है। इन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति का जन्म होता है।
किसी भी कार्य की स्थिति पहले विचार रूप में ही होती है। उसके बिना वह कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम जो भी कार्य करना चाहते हों उसके लिए दृढ़ विचार करना, यही मुख्य और आरम्भिक कदम है। मन्दतापूर्वक उत्पन्न होने वाला विचार मन्द परिणाम ही उत्पन्न करता है। विचार मजबूत ही होना चाहिए, अन्यथा जैसी चाहिए वैसी कार्य सिद्धि नहीं होगी।
संसार के समस्त महान कार्यों का मूल ऐसी मजबूत इच्छा और कल्पना में रहता है, जो निराशा और निरुत्साह की परिस्थितियां आ जाने पर भी टिकी रहती हैं और उसके लिए मनुष्य बलिदान करने को तैयार रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ‘‘तुम्हारी श्रद्धा के अनुरूप ही तुमको सफलता प्राप्त होगी।’’ हम जीवन द्वारा कितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसका पता हमारी श्रद्धा से ही ठीक-ठीक लग सकता है। थोड़ी श्रद्धा वाले मनुष्य को थोड़ा मिलता है और अधिक श्रद्धा वाले को अधिक मिलता है।
अगर हम स्वावलम्बी मनुष्यों की सफलताओं के विषय में जांच करेंगे तो हमें यही विदित होगा कि उन्होंने जब किसी विषय में उद्योग आरम्भ किया था, तब वे अपने उठाए हुए काम के विषय में दृढ़ और अचल श्रद्धा रखते थे। अपने ध्येय में उनका मन इतनी मजबूती से संलग्न था कि अपने व्यक्तित्व और शक्ति में कम विश्वास रखने वाले मनुष्यों के मार्ग में जो बाधायें आती हैं, वे उनके सम्मुख से पहले ही हट गई थीं, संसार ने उनके लिए रास्ता दिया था। भाग्यदेवी मानो उन पर परम प्रसन्न थी। इस प्रकार उन्होंने जिस किसी रोजगार में हाथ डाला उसी में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। हम उनके सम्बन्ध में तरह-तरह के अनुमान करते रहते हैं, परन्तु वास्तव में उनको जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण यही था कि वे अपनी आशा के सम्बन्ध में निरन्तर सृजनात्मक और निश्चयात्मक विचार करते रहते थे।
हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे यही हमको मानना चाहिए। इतना ही नहीं इस पर पूर्ण अन्तःकरण से विश्वास रखना चाहिए। शिथिल महत्वाकांक्षा और ढीले प्रयत्न से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारी श्रद्धा में, हमारे निश्चय में, हमारे उद्योग में बल होना चाहिए। हमको कार्य सिद्धि करने वाली शक्ति के साथ ही किसी विषय का निश्चय करना चाहिए।
जिस प्रकार बहुत अधिक गर्मी देने से लोहा पिघल जाता है, जिस प्रकार विद्युत की एकाग्र शक्ति सब वस्तुओं से अधिक कठोर हीरा को भी घिस डालती है, उसी प्रकार एकाग्र लक्ष्य और अजेय उद्देश्य सफलता प्राप्त कराता है। आधे मन से किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।
जो कभी पीछे की तरफ नहीं देखता, पराजय का विचार भी नहीं करता और लक्ष्य सिद्धि के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहता है, वही मनुष्य दृढ़ निश्चय कर सकता है। एक व्यक्ति जब आत्म-श्रद्धा को खो देता है—हथियार डाल देता है, तो उसका उपाय यही है कि उसकी खोई हुई वस्तु—आत्म श्रद्धा को उसे पुनः प्राप्त कराने का प्रयत्न करना चाहिए। उस समय ऐसा विचार मत करो कि ‘‘उसका भाग्य उसे जहां-तहां भटका रहा है, और इस रहस्यमय भाग्य के सामने उसका क्या वश चल सकता है।’’ उसको मन से निकाल देने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी तरह के भाग्य से मनुष्य बड़ा है और बाहर की किसी भी शक्ति की अपेक्षा प्रचण्ड शक्ति उसके भीतर मौजूद हैं। इस बात को जब तक वह नहीं समझ लेगा तब तक उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता।
बहुत से लोगों का जीवन अत्यन्त संकुचित और दरिद्री होता है, उसका कारण यही है कि उनमें आत्म श्रद्धा और कार्य करने की श्रद्धा नहीं होती। बहुत से लोग इस तरह फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं और किसी प्रकार का साहस करने में इतना डरते रहते हैं कि उनका आगे बढ़ सकना कठिन ही होता है। आत्म-श्रद्धा और ईश्वर-श्रद्धा मनुष्य के दो महान शक्तिस्रोत हैं।
आत्म-श्रद्धा का अर्थ अहंकार नहीं वरन् ज्ञान समझना चाहिए। अपने आरम्भ किये हुए काम को पूरा करने की शक्ति हम में मौजूद है ऐसा प्रतीत होने से यह ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारी समस्त उन्नति और संस्कृति इसी आत्म-श्रद्धा पर आधारित होती है। इसके विपरीत जिन मनुष्यों के मन में सदा शंका घुसी रहती है और जो हानि-लाभ की गिनती करने में ही लगे रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं हो सकती। यदि वे कभी कार्यारम्भ भी करते हैं तो डगमगाते हुए चलते हैं, उनके कार्य में बल नहीं होता, उनके उद्योग में निश्चय का भाव नहीं पाया जाता।
कार्य सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रचण्ड बल से कार्य आरम्भ करना चाहिए, और सदा सामने आने वाले विघ्नों को हटाने की शक्ति रखनी चाहिए। यह उद्देश्य डगमगाते, शंकाशील, अस्थिर मन से सिद्ध नहीं हो सकता। जो कार्य अन्य लोगों को असम्भव जान पड़ता है उसे ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कर सकने का पूरा विश्वास रखता है। इससे ज्ञात होता है कि उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उसके आरम्भ किये हुए कार्य को सिद्ध करने का बल देती है।
श्रद्धा ही मनुष्य को अनन्त के साथ संयुक्त कर देती है। और जब मनुष्य परमात्मा के इतने निकट रहता है कि उसे सदा उसके उपस्थित होने का अनुभव हुआ करता है, तो वह आवश्यकता पड़ने पर असामान्य शक्ति दिखला सकता है। आत्म-श्रद्धा और ईश्वर-श्रद्धा से मनुष्य की शक्ति में जितनी वृद्धि होती है उतनी और किसी वस्तु से नहीं होती। आत्म-श्रद्धा से एक ही काम जानने वाला सफलता प्राप्त कर लेता है जबकि उसके बिना दस काम जानने वाला भी निष्फल सिद्ध होता है।
श्रद्धा में चमत्कार करने की शक्ति है। धर्म-शास्त्रों में चमत्कारी व्यक्तियों की जो घटनायें लिखी हैं उनका रहस्य आत्म-श्रद्धा में ही समाया हुआ है। मनुष्य की आत्म-श्रद्धा प्रकट करती है कि उस व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति मौजूद है जो या तो मार्ग में आने वाले विघ्नों का नाश कर देगी या उनको ऐसा नगण्य बना देगी कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।
श्रद्धा द्वार को खोल देती है, वह हमें आत्मा की अनन्त शक्तियों को देखने के लिए शक्तिमान करती है, वह आत्मा के ऐसे अजेय बल को प्रकट करती है, कि उससे हमको अपनी आन्तरिक शक्ति में स्पष्ट रूप से वृद्धि होती जान पड़ती है। कारण यह है कि उस अवस्था में हम सर्वशक्तिमान प्रभु को स्पर्श करते रहते हैं, सब पदार्थों का जो मूल कारण है उसकी झांकी हमको होती रहती है।
श्रद्धा ऐसी वस्तु है कि वह अनुमान नहीं करती वरन् निश्चय कर लेती है। जिस वस्तु को हमारी स्थूल प्रकृति (पशु-प्रकृति) नहीं जान सकती, उसे जानने की समर्थ श्रद्धा ही प्रदान करती है। वह हमारे भीतर रहने वाला एक ऋषि अथवा सन्देश-वाहक है। वह आजीवन साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करती है। वह मनुष्य को हिम्मत हारने और उद्योग से विमुख हो जाने से रोककर उसकी अन्तःशक्ति का दर्शन कराती है।
अगर हममें ईश्वर के प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा हो तो हम कठिनाइयों के पर्वतों को हटा सकते हैं। ऐसी श्रद्धा जीवन पर्यन्त, अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक बनी रहती है। अगर हममें भरपूर श्रद्धा हो तो हम अपने समस्त क्लेशों को दूर कर सकते हैं और अनेक विशेष कामों को पूरा करके दिखा सकते हैं।
श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती। वह चमत्कार करके दिखा सकती है। वह समस्त सीमाओं के पार देख सकती है, सब प्रकार की संकुचितताओं को उलांघ सकती है, समस्त विघ्नों को नष्ट करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।
शंका और भय, डरपोकपन और कायरता हमको घटिया और मामूली दशा में रखते हैं। जबकि हम ऊंचे दर्जे के काम करने की शक्ति रखते हैं तब भी हम इन शंका आदि दोषों के कारण तुच्छ कार्य करते रहते हैं।
यदि हमारे भीतर यथोचित श्रद्धा हो, तो हम इस समय ईश्वर की तरफ जितनी गति कर रहे हैं, उससे बहुत अधिक गति से उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। आगे चलकर अवश्य ही ऐसा समय आएगा, जो प्रत्येक मानव में अपार श्रद्धा का अस्तित्व होगा और वह विजयी जीवन व्यतीत करेगा। उस समय जगत में हीनता और निष्फलता नहीं रहेगी और जीवन की समस्त अशान्ति का लोप हो जाएगा।
आन्तरिक शक्ति की समस्या और समाधान—
एक मनुष्य के पास पर्याप्त साधन, सम्पत्ति जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, फिर भी वह अशान्त, परेशान-सा दिखाई देता है। दूसरा उच्च शिक्षा सम्पन्न अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी भूला-भटका-सा दिखाई देता है। व्यापारी, विद्वान्, नेता, पण्डित उच्च पद पर आसीन लोग इसी एक प्रश्न के समाधान के लिए परेशान मालूम पड़ते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत है—संघर्ष, अशान्ति, क्लेश, परेशानी। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान हैं और तरह-तरह के प्रश्न करते हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं होता।
वस्तुतः जीवन के इस प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं या संसार में नहीं है। इसका समाधान मनुष्य के अपने अन्दर है। वह है—जीवन व्यवहार में हृदय को महत्व देना। हमारी बुद्धि बढ़ी है, किन्तु हमारा हृदय अभी तक जड़ ही बना हुआ है। बुद्धि के बल पर व्यापार, शिक्षा, पाण्डित्य विद्वत्ता, उच्च पद एवं जीवन की अन्य सभी तरह की सफलताएं मिल जाती हैं, किन्तु हृदय की व्यापकता विशालता के अभाव में ये सफलताओं के बड़े-बड़े महल, उसी तरह डरावने और अटपटे लगते हैं जैसे सुनसान अन्धेरे भवन और किले। हृदय की जीवनी-शक्ति के अभाव में मनुष्य की समस्त समृद्धि, विद्वता, बड़प्पन, उच्च पद के भयावने भूत उसे ही खाने लगते हैं।
उस समय महात्मा बुद्ध को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। वे राजपुत्र थे, और सभी कुछ थे, किन्तु बुद्ध को ये सब अटपटे लगे। आत्म प्रसाद, शान्ति, आनन्द का समाधान बुद्ध को इस समृद्धि और राजमहल में नहीं मिला। वे इन सब अलंकारों को छोड़कर नीचे उतरे, अपनी इन दीवारों को तोड़ बुद्ध व्यापक बने, जन-मन के साथ एकता प्राप्त की और वे फिर राजमहल के राजकुमार न रह कर असीम के साथ—मानवता के साथ एकाकार हुए, तभी उन्हें जीवन के उस प्रश्न का समाधान मिला।
भगवान राम ने इसी पथ का वरण किया। समृद्ध-सुसम्पन्न अयोध्या नगरी को त्याग राम वल्कल वस्त्र धारण कर अनन्त पथ के पथिक बने और जंगल में कृत्रिमता से दूर प्रकृति के फैले विशाल आंचल में पशु-पक्षी, वनस्पति, नदी, नालों, पहाड़ तक से अपने हृदय को जोड़ा। शबरी, गिद्ध, केवट के हृदय से हृदय जोड़ने वाले दशरथ सुत राम जन-मानस के राम बन गए।
महात्मा गांधी ने उच्च शिक्षा का अभिमान छोड़ा, जनता-जनार्दन के समकक्ष उतरे, वैसा ही पहना, वैसा ही खाया। अपने जीवन को, अपनी विद्वत्ता को निजी समृद्धि का आधार न बनाकर पीड़ित मानवता के कल्याण, उन्नति, प्रगति का आधार बनाया।
इसी तरह स्वामी रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द, रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, मालवीय जी आदि ने अपनी समृद्धि, विद्वत्ता, पाण्डित्य, उच्च पद आदि से नीचे उतर मानवता के हृदय से अपना हृदय जोड़ा। मानवता के कष्ट-दुःख अपने कष्ट-दुःख समझे, जनता जनार्दन की पीड़ा अपनी पीड़ा समझी और उसके लिए अपने जीवन को लगाया। एक घोर लोकसंग्रही से भी अधिक श्रम किया, कष्ट झेले, परेशानी उठाई पीड़ित, दुःखी क्लान्त मानवता के लिए। जनता-जनार्दन के लिए।
समृद्धि, रूप, पाण्डित्य, विद्वत्ता, पद आदि का अभिमान ही वह चहार-दीवारी है जो हमें जीवन के यथार्थ रूप से दूर किए हुए है। अभिमान अहंकार चाहे वह किसी भी गुण, रूप, वस्तु का क्यों न हो, मनुष्य के वास्तविक सुख और आत्म-प्रसाद से उसको दूर रखता है। जिसके दिल और दिमाग इस दम्भ की घेराबन्दी में जकड़े हुए हैं वह कैसे सन्तुष्ट रह सकता है?
जब धनवान अपने धन का, दानवृत्ति का अभिमान छोड़कर दरिद्रता के प्रति अपने हृदय को जोड़ लेगा, शिक्षाशास्त्री पण्डित जब मानवता की पंक्ति में आकर बैठेंगे, उच्च पद सम्पन्न लोग जब जनता जनार्दन की अर्चना में लगेंगे, तो उनका अहंभाव सहज ही तिरोहित हो जायगा और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान मिल सकेगा। जीवन का सच्चा सुख आत्म प्रसाद, आत्म-शान्ति, सन्तोष हृदय को मुक्त और व्यापक बनाने से ही सम्भव है।
राजा भर्तृहरि ने कहा था—‘‘न राजा बड़ा है न तपस्वी, न विद्वान्, जो अपने जीवन और कार्यों से सन्तुष्ट है वही सबसे बड़ा है।’’
स च भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाल ।
मनसि च परितुष्टे, कोऽर्थवान् को दरिद्रः ।।
‘जिसको तृष्णा अधिक है वही दरिद्री है। जिसका चित्त सन्तुष्ट है, उसके सामने न कोई धनी है न दरिद्री।’
मानव-मानव के बीच इस संघर्ष-लड़ाई का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं वरन् तेरे-मेरे का प्रश्न है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपने की सार-सम्भाल सभी को प्रिय लगती है, किन्तु दूसरे के साथ वह भाव नहीं। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरे से अपना जितना लाभ बन सके इनके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है।
इस व्यापक सफलता का भी एक समाधान है वह यह है कि अपने हृदय को मेरे-तेरे के संकीर्ण घेरे से निकाल कर ‘समग्र’ के साथ जोड़ा जाय। इसके व्यावहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है—सहअस्तित्व का मन्त्र। स्वयं जियें और दूसरों को जीने दें। अपनी-अपनी थाली में ही सब बैठकर खायें। इसके बाद ही दूसरा मन्त्र है—‘‘दूसरे के जीने के लिए मुझे सहयोग करना होगा।’’ जिसकी पराकाष्ठा अपने आपको मिटा देने तक रहती है। दूसरों के जीने के लिए अपने आपको मिटाने की भावना एक दूसरे के दिल और दिमाग को जोड़ती है, एकाकार करती है। यही व्यक्ति से लेकर विश्व समस्या का मूल समाधान है।
हम भी अपने हृदय को दूसरों के लिए इसी तरह सम्वेदनशील बनाकर अपनी और विश्व की समस्याओं के समाधान में योग दे सकते हैं। जब परिवार में हम अपने लिए अच्छी मांग न रखकर दूसरों का ध्यान रखेंगे तो क्यों नहीं हमारा परिवार स्वर्गीय बनेगा? इसी तरह पड़ोस, देश, समाज, जाति की यही आवश्यकता है जिसे अनुभव किए बिना मानव और विश्व की समस्या का समाधान न हो सकेगा।
हृदय की सम्वेदना का विस्तार ही मनुष्य को भगवान के समकक्ष पहुंचाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस की अत्युच्च कोटि की सम्वेदनशीलता ने उन्हें काली-मय और भगवान बना दिया। सामान्यतः लोगों में यह सम्वेदना बीज अधाखिला, अधफला ही रहता है। अपनों के अपनत्व के दायरे में सीमित किए हुए लोग साधारण मनुष्य ही बनकर रह जाते हैं।
आत्म-विश्वास और ईश्वर-विश्वास ये मनुष्य के दो महान अवलम्बन हैं। जब सम्वेदना को संकीर्णता और विकृति की कालकोठरी में डालकर क्रूरता-कठोरता और पापाचार को ही अपनी प्रकृति बना लिया जाता है, तो व्यक्ति शैतान के रूप में ढल जाता है। वह न केवल भगवान से दूर हो जाता है अपितु अपने भीतर की मनुष्यता को भी मार डालता है।
करुणा निधान भगवान ने तो हमें अपने समकक्ष बन सकने के सभी साधन और शक्तिस्रोत दिए हैं, अब हम क्या बनते हैं—शैतान, इन्सान या भगवान, यह हमारी आकांक्षा, संकल्प एवं प्रयत्न-पुरुषार्थ की दिशा तथा स्वरूप पर निर्भर करता है।
यदि हम आत्म-विश्वास और ईश्वर-विश्वास से विरत हो गए, तो शैतानियत हमें गले लगा लेगी, यदि आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे तो इन्सानियत कभी भी भूलेगी नहीं और यदि आत्म-विश्वास एवं ईश्वर-विश्वास दोनों का प्रकाश जीवन में व्याप्त हो गया, तो देवत्व दूर नहीं रहेगा।