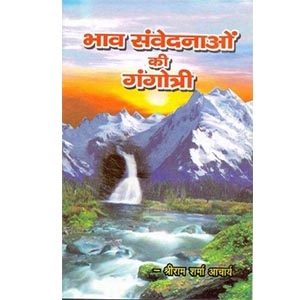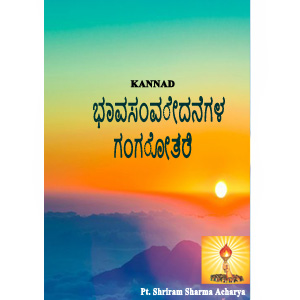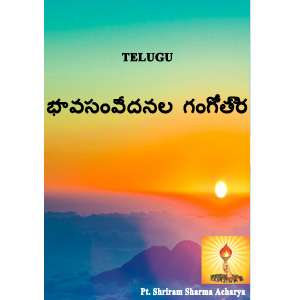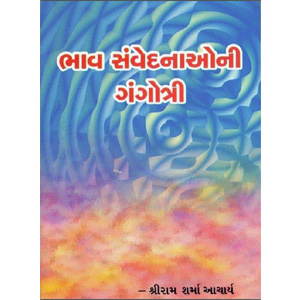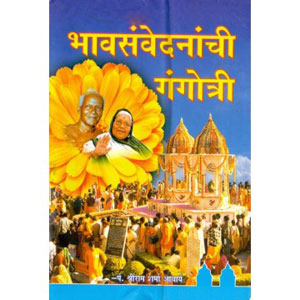भाव संवेदनाओं की गंगोत्री 
वेदव्यास की अंतर्व्यथा
Read Scan Version
‘‘आपके चेहरे पर खिन्नता के चिह्न!’’ आगंतुक ने सरस्वती नदी के तट पर, आश्रम के निकट बैठे हुए मनीषी के मुखमंडल पर छाए भावों को पढ़ते हुए कहा। इधर विगत कई दिनों से वह व्यथित थे। नदी के तट पर बैठकर घंटों विचारमग्न रहना, शून्य की ओर ताकते रहना, उनकी सामान्य दिनचर्या बन गई थी। आज भी कुछ उसी प्रकार बैठे थे।
आगंतुक के कथन से विचार-शृंखला टूटी। ‘‘अरे! देवर्षि आप?’’ चेहरे पर आश्चर्य व प्रसन्नता की मिली-जुली अभिव्यक्ति झलकी।
‘‘पर आप व्यथित क्यों हैं?’’ उन्होंने पास पड़े आसन पर बैठते हुए कहा-पीड़ा-निवारक को पीड़ा, वैद्य को रोग? कैसी विचित्र स्थिति है?’’
‘‘विचित्रता नहीं विवशता कहिए। इसे उस अंतर्व्यथा के रूप में समझिए, जो पीड़ा-निवारक को सामने पड़े पीड़ित को देखकर, उसके कष्ट हरने में असफल होने पर होती है। वैद्य को उस समय होती है, जब वह सामने पड़े रोगी को स्वस्थ कर पाने में असफल हो जाता है।’’
कुछ रुककर उन्होंने गहरी श्वाँस ली और पुन: वाणी को गति दी-व्यक्ति और समाज के रूप मेें मनुष्य सन्निपात के रोग से ग्रस्त है। कभी हँसता है, कभी कुदकता-फुदकता है; कभी अहंकार के ठस्से में अकड़ा चलता है। परस्पर का विश्वास खो जाने पर आचार-विचार का स्तर कैसे बने? जो थोड़ा-बहुत दिखाई देता है, वह अवशेषों का दिखावा भर है।
‘‘और परिवार...............इतना कहकर उनके मुख पर एक क्षीण मुस्कान की रेखा उभरी, नजर उठाकर सामने बैठे, देवर्षि की ओर देखा ‘‘इनकी तो और भी करुण दशा है। इनमें मोह रह गया है, प्रेम मर गया है। मोह भी तब तक, जब तक स्वार्थ सधे। विवाहित होते ही संतानें माँ-बाप को तिलांजलि दे देती हैं। सारी रीति ही उलटी है? उठे को गिराना, गिरे को कुचलना, कुचले को मसलना, यही रह गया है। आज मनुष्य और पशु में भेद आचार-विचार की दृष्टि से नहीं वरन् आकार-प्रकार की दृष्टि से है।’’ कहते-कहते ऋषि का चेहरा विवश हो गया। भावों को जैसे-तैसे रोकते हुए धीरे से कहा-देवता बनने जा रहा मनुष्य, पशु से भी गया-गुजरा हो रहा है।’’
‘‘महर्षि व्यास ! आप तो मनीषियों के मुकुटमणि हैं।’’ जैसे कुछ सोचते हुए देवर्षि ने कहा-आपने प्रयास नहीं किए?’’
‘‘प्रयास!......प्रयास किए बिना भला जीवित कैसे रहता जो भटकी मानवता को राह सुझाने हेतु प्रयत्नरत नहीं है, हाथ-पर हाथ धरे बैठा है, स्वयं की बौद्धिकता के अहं से ग्रस्त है, उसे मनीषी कहलाने, यहाँ तक कि जीवित रहने का भी हक नहीं है।’’
‘‘किस तरह के प्रयास किए?’’
‘‘मानवीय बुद्घि के परिमार्जन हेतु प्रयास। इसके लिए वैदिक मंत्रों का पुन: वर्गीकरण किया। कर्मकाण्डों का स्वरूप सँवारा, ताकि मंत्रों में निहित दिव्य-भावों को ग्रहण करने में सुभीता हो; पर........।’’
‘‘पर क्या?’’
‘‘प्राणों को छोड़कर लोग सिर्फ कर्मकाण्डों के कलेवर से चिपट गए। वेद, अध्ययन की जगह पूजा की वस्तु बन गए। यहीं तक सीमित रहता, तब भी गनीमत थी। इनकी ऊटपटांग व्याख्याएँ करके, जाति-भेद की दीवारें खड़ी की जाने लगीं।
‘‘फिर .......?’’
‘‘ पुराणों की रचना की, जिसका उद्देश्य था, वेद में निहित सत्य-सद्विचार को कथाओं के माध्यम से जन-जन के गले उतारा जा सके, जिससे बौद्धिकता के उन्माद का शमन हो । किंतु.......।’’
‘‘किंतु क्या?’’
‘‘यह प्रयास भी आंशिक सफल रहा। सहयोगियों ने स्मृतियाँ रचीं, पर यह सब बुद्धिमानों के जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गए, जन-जन के मानस में फेर-बदल करने का अभियान पूरा नहीं हुआ। बुद्धि सुधरी नहीं, अहं गया नहीं, परिणाम महाभारत के युद्धोन्माद के रूप में सामने आया। विज्ञान, धन का गुलाम और धन दुर्बुद्धि के हाथ की कठपुतली; सारे साधन इसी के इर्द-गिर्द अपने को ज्ञानी कहने व विद्वान-बुद्धिमान-बलवान् समझने वाले, सभी दुर्बुद्धि के दास सिद्ध हुए। देश और समाज का वैभव एक बार फिर चकनाचूर हुआ, पर मैं अकेले चलता रहा-प्रयासों में शिथिलता नहीं आने दी।’’ महर्षि के स्वर में उत्साह था और देवर्षि के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी।
कुछ रुककर बोले-महाभारत की रचना की, मानवीय कुकृत्यों की वीभत्सता का चित्रण किया। सत्कर्मों की राह दिखाई, वह सभी कुछ ढूँढ़कर सँजोया, जिसका अवलंबन ले मानव सुधर सके-सँवर सके। बुद्धि ,विगत से सीख सके; पर परिणाम वही-ढाक के तीन पात।’’
तो क्या प्रयास से विरत हो गए महर्षि-देवर्षि का स्वर था। नहीं-विरत क्यों होता? कर्तव्यनिष्ठा का ही दूसरा नाम मनुष्यता है। एक मनीषी का जो कर्तव्य है, वह अंतिम साँस तक अनवरत करता रहूँगा।’’
‘‘सचमुच यही है निष्ठा?’’
‘‘हाँ तो ‘महाभारत’ का समुचित प्रभाव न देखकर यह सोच उभरी कि शायद, इतने विस्तृत ग्रंथ को लोग समयाभाव के कारण पढ़ न सके हों? इस कारण ब्रह्मसूत्र की रचना की। सरल सूत्रों से जीवन-जीने के आवश्यक तत्त्वों को सँजोया। एकता-समता की महत्ता बताई। एक ही परमसत्ता हर किसी में समाहित है- कहकर, भाईचारे की दिव्यता तुममें है- कहकर स्वयं को दिव्य बनाने, अपना उद्धार करने की प्रेरणा दी, पर हाय री मानवी बुद्धि! तूने ग्रहणशीलता तो जैसे सीखी ही नहीं। पंडिताभिमानियों ने इस पर बुद्धि की कलाबाजियाँ खाते हुए तरह-तरह के भाष्य लिखने शुरू कर दिए, शास्त्रार्थ की कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। जीवन-जीने के सूत्रों का यह ग्रंथ अखाड़ा बनकर रह गया।
‘‘अब पुन: समाधान की तलाश में हूँ। अंतर्व्यथा का कारण यह नहीं है कि मेरे प्रयास असफल हो गए। अपितु मानव की दुर्दशा, दुर्मति-जन्य दुर्गति देखी नहीं जाती । असह्य बेचैनी है अंदर, पर क्या करूँ? राह नहीं सूझ रही।’’ कहकर वह आशाभरी नजरों से देवर्षि की ओर देखने लगे।
आगंतुक के कथन से विचार-शृंखला टूटी। ‘‘अरे! देवर्षि आप?’’ चेहरे पर आश्चर्य व प्रसन्नता की मिली-जुली अभिव्यक्ति झलकी।
‘‘पर आप व्यथित क्यों हैं?’’ उन्होंने पास पड़े आसन पर बैठते हुए कहा-पीड़ा-निवारक को पीड़ा, वैद्य को रोग? कैसी विचित्र स्थिति है?’’
‘‘विचित्रता नहीं विवशता कहिए। इसे उस अंतर्व्यथा के रूप में समझिए, जो पीड़ा-निवारक को सामने पड़े पीड़ित को देखकर, उसके कष्ट हरने में असफल होने पर होती है। वैद्य को उस समय होती है, जब वह सामने पड़े रोगी को स्वस्थ कर पाने में असफल हो जाता है।’’
कुछ रुककर उन्होंने गहरी श्वाँस ली और पुन: वाणी को गति दी-व्यक्ति और समाज के रूप मेें मनुष्य सन्निपात के रोग से ग्रस्त है। कभी हँसता है, कभी कुदकता-फुदकता है; कभी अहंकार के ठस्से में अकड़ा चलता है। परस्पर का विश्वास खो जाने पर आचार-विचार का स्तर कैसे बने? जो थोड़ा-बहुत दिखाई देता है, वह अवशेषों का दिखावा भर है।
‘‘और परिवार...............इतना कहकर उनके मुख पर एक क्षीण मुस्कान की रेखा उभरी, नजर उठाकर सामने बैठे, देवर्षि की ओर देखा ‘‘इनकी तो और भी करुण दशा है। इनमें मोह रह गया है, प्रेम मर गया है। मोह भी तब तक, जब तक स्वार्थ सधे। विवाहित होते ही संतानें माँ-बाप को तिलांजलि दे देती हैं। सारी रीति ही उलटी है? उठे को गिराना, गिरे को कुचलना, कुचले को मसलना, यही रह गया है। आज मनुष्य और पशु में भेद आचार-विचार की दृष्टि से नहीं वरन् आकार-प्रकार की दृष्टि से है।’’ कहते-कहते ऋषि का चेहरा विवश हो गया। भावों को जैसे-तैसे रोकते हुए धीरे से कहा-देवता बनने जा रहा मनुष्य, पशु से भी गया-गुजरा हो रहा है।’’
‘‘महर्षि व्यास ! आप तो मनीषियों के मुकुटमणि हैं।’’ जैसे कुछ सोचते हुए देवर्षि ने कहा-आपने प्रयास नहीं किए?’’
‘‘प्रयास!......प्रयास किए बिना भला जीवित कैसे रहता जो भटकी मानवता को राह सुझाने हेतु प्रयत्नरत नहीं है, हाथ-पर हाथ धरे बैठा है, स्वयं की बौद्धिकता के अहं से ग्रस्त है, उसे मनीषी कहलाने, यहाँ तक कि जीवित रहने का भी हक नहीं है।’’
‘‘किस तरह के प्रयास किए?’’
‘‘मानवीय बुद्घि के परिमार्जन हेतु प्रयास। इसके लिए वैदिक मंत्रों का पुन: वर्गीकरण किया। कर्मकाण्डों का स्वरूप सँवारा, ताकि मंत्रों में निहित दिव्य-भावों को ग्रहण करने में सुभीता हो; पर........।’’
‘‘पर क्या?’’
‘‘प्राणों को छोड़कर लोग सिर्फ कर्मकाण्डों के कलेवर से चिपट गए। वेद, अध्ययन की जगह पूजा की वस्तु बन गए। यहीं तक सीमित रहता, तब भी गनीमत थी। इनकी ऊटपटांग व्याख्याएँ करके, जाति-भेद की दीवारें खड़ी की जाने लगीं।
‘‘फिर .......?’’
‘‘ पुराणों की रचना की, जिसका उद्देश्य था, वेद में निहित सत्य-सद्विचार को कथाओं के माध्यम से जन-जन के गले उतारा जा सके, जिससे बौद्धिकता के उन्माद का शमन हो । किंतु.......।’’
‘‘किंतु क्या?’’
‘‘यह प्रयास भी आंशिक सफल रहा। सहयोगियों ने स्मृतियाँ रचीं, पर यह सब बुद्धिमानों के जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गए, जन-जन के मानस में फेर-बदल करने का अभियान पूरा नहीं हुआ। बुद्धि सुधरी नहीं, अहं गया नहीं, परिणाम महाभारत के युद्धोन्माद के रूप में सामने आया। विज्ञान, धन का गुलाम और धन दुर्बुद्धि के हाथ की कठपुतली; सारे साधन इसी के इर्द-गिर्द अपने को ज्ञानी कहने व विद्वान-बुद्धिमान-बलवान् समझने वाले, सभी दुर्बुद्धि के दास सिद्ध हुए। देश और समाज का वैभव एक बार फिर चकनाचूर हुआ, पर मैं अकेले चलता रहा-प्रयासों में शिथिलता नहीं आने दी।’’ महर्षि के स्वर में उत्साह था और देवर्षि के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी।
कुछ रुककर बोले-महाभारत की रचना की, मानवीय कुकृत्यों की वीभत्सता का चित्रण किया। सत्कर्मों की राह दिखाई, वह सभी कुछ ढूँढ़कर सँजोया, जिसका अवलंबन ले मानव सुधर सके-सँवर सके। बुद्धि ,विगत से सीख सके; पर परिणाम वही-ढाक के तीन पात।’’
तो क्या प्रयास से विरत हो गए महर्षि-देवर्षि का स्वर था। नहीं-विरत क्यों होता? कर्तव्यनिष्ठा का ही दूसरा नाम मनुष्यता है। एक मनीषी का जो कर्तव्य है, वह अंतिम साँस तक अनवरत करता रहूँगा।’’
‘‘सचमुच यही है निष्ठा?’’
‘‘हाँ तो ‘महाभारत’ का समुचित प्रभाव न देखकर यह सोच उभरी कि शायद, इतने विस्तृत ग्रंथ को लोग समयाभाव के कारण पढ़ न सके हों? इस कारण ब्रह्मसूत्र की रचना की। सरल सूत्रों से जीवन-जीने के आवश्यक तत्त्वों को सँजोया। एकता-समता की महत्ता बताई। एक ही परमसत्ता हर किसी में समाहित है- कहकर, भाईचारे की दिव्यता तुममें है- कहकर स्वयं को दिव्य बनाने, अपना उद्धार करने की प्रेरणा दी, पर हाय री मानवी बुद्धि! तूने ग्रहणशीलता तो जैसे सीखी ही नहीं। पंडिताभिमानियों ने इस पर बुद्धि की कलाबाजियाँ खाते हुए तरह-तरह के भाष्य लिखने शुरू कर दिए, शास्त्रार्थ की कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। जीवन-जीने के सूत्रों का यह ग्रंथ अखाड़ा बनकर रह गया।
‘‘अब पुन: समाधान की तलाश में हूँ। अंतर्व्यथा का कारण यह नहीं है कि मेरे प्रयास असफल हो गए। अपितु मानव की दुर्दशा, दुर्मति-जन्य दुर्गति देखी नहीं जाती । असह्य बेचैनी है अंदर, पर क्या करूँ? राह नहीं सूझ रही।’’ कहकर वह आशाभरी नजरों से देवर्षि की ओर देखने लगे।